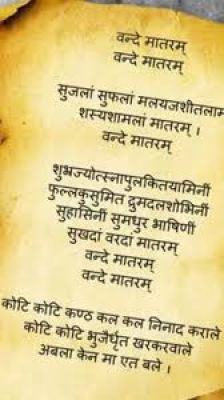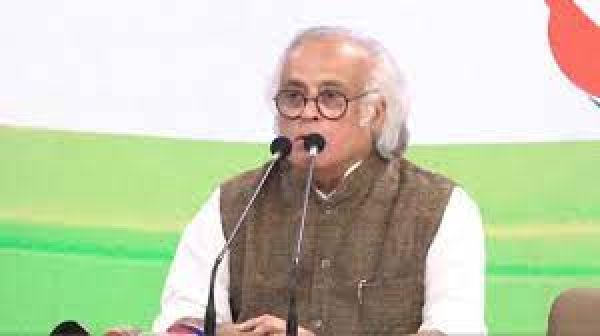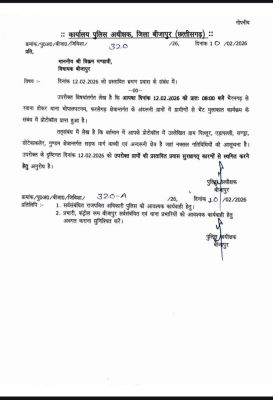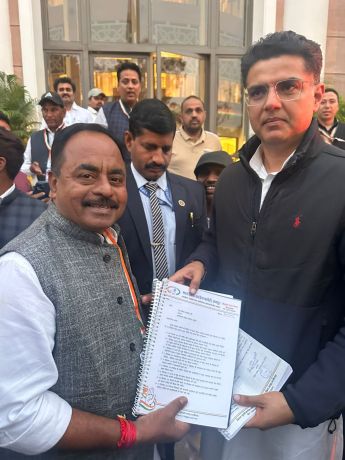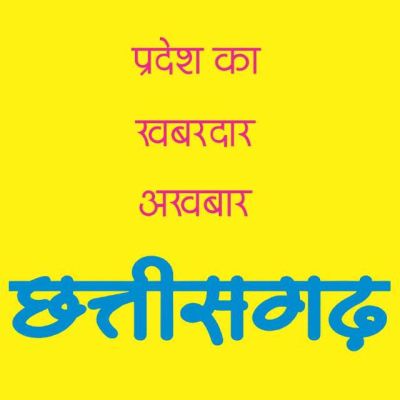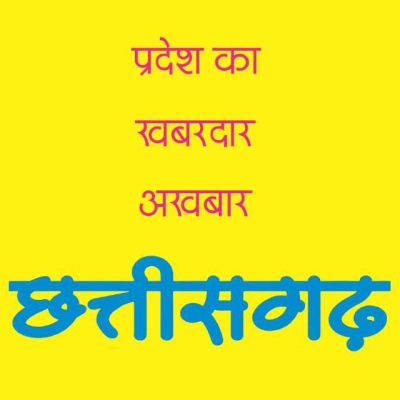न्यूर्नबर्ग (जर्मनी), 11 फरवरी। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत ने व्यापार समझौतों में हमेशा उन क्षेत्रों को लेकर ‘‘स्पष्ट सोच’’ रखी है जो देश के लिए ‘‘बेहद’’ संवेदनशील हैं और अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते में ऐसे सभी प्रमुख क्षेत्रों की पूरी तरह रक्षा की गई है।
उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष संयुक्त बयान को कानूनी समझौते में बदलने पर काम कर रहे हैं जिसे मार्च के अंत तक अंतिम रूप देकर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।
अग्रवाल ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘ भारत ने हमेशा सभी समझौतों पर स्पष्ट सोच के साथ बातचीत की है। जो भी क्षेत्र भारत के लिए बेहद संवेदनशील हैं, जहां हमें लगता है कि हमारे किसान, मछुआरे, दुग्ध क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, वहां हमने अपने साझेदार देशों को साफ बता दिया है कि भारत ऐसे मामलों में बाजार नहीं खोल सकता या पहुंच नहीं दे सकता।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ अगर आप पिछले एक साल में किए गए सभी समझौतों को देखें। हमने पांच व्यापार समझौते किए हैं। सभी में संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा की गई है। अमेरिका के साथ भी सभी प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखा गया है। जहां थोड़ी संवेदनशीलता थी, वहां हमने शुल्क दर ‘कोटा’ व्यवस्था का इस्तेमाल किया ताकि बाजार तक पहुंच सीमित रहे और हमारे किसानों पर असर न पड़े।’’
इस महीने की शुरुआत में घोषित अंतरिम व्यापार समझौते के तहत भारत ने मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल (ईंधन), तंबाकू, कुछ सब्जियों और मांस जैसे संवेदनशील कृषि एवं दुग्ध उत्पादों को पूरी तरह संरक्षित रखा है। इन वस्तुओं पर अमेरिका को कोई शुल्क रियायत नहीं दी गई है।
ये उत्पाद संवेदनशील हैं क्योंकि इनका संबंध देश के छोटे एवं सीमांत किसानों की आजीविका से है।
अन्य मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में भी भारत ने संवेदनशील कृषि और दुग्ध उत्पादों पर आयात शुल्क में कोई रियायत नहीं दी है। भारत ने हाल ही में यूरोपीय संघ, ब्रिटेन तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए को अंतिम रूप दिया है।
कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियां जैसे पशुपालन भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इनसे 50 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जहां कृषि अत्यधिक मशीनीकृत और कॉरपोरेट आधारित है, वहीं भारत में यह आजीविका का सवाल है।
भारतीय कृषि क्षेत्र को वर्तमान में घरेलू किसानों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए मध्यम से उच्च शुल्क एवं नियामकीय उपायों के जरिये संरक्षण दिया गया है।
भारत को 2024 में अमेरिका का कृषि निर्यात 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। प्रमुख निर्यातों में बादाम (छिलके सहित, 86.8 करोड़ डॉलर), पिस्ता (12.1 करोड़ डॉलर), सेब (2.1 करोड़ डॉलर) और एथेनॉल (एथिल अल्कोहल, 26.6 करोड़ डॉलर) शामिल हैं।
अग्रवाल यहां ‘बायोफैच’ 2026 प्रदर्शनी में हिस्सा लेने पहुंचे हैं जहां 100 से अधिक भारतीय प्रदर्शक और करीब 20 राज्य अपने जैविक उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। यूरोपीय संघ इन उत्पादों का बड़ा बाजार है।
उन्होंने कहा, ‘‘ दल इस पर काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि मार्च तक इसे (अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते को) औपचारिक रूप दे दिया जाएगा।’’
श्रम-प्रधान क्षेत्रों के बारे में उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ यह समझौता भारत को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बढ़त देगा, क्योंकि अमेरिकी बाजार में उन देशों पर भारत से अधिक शुल्क लगाया जा रहा है।
भारत पर जवाबी शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत किया जाएगा, जबकि चीन के लिए यह 35 प्रतिशत और वियतनाम के लिए 20 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा, ‘‘ चूंकि अमेरिका श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए एक मजबूत बाजार रहा है, इसलिए इस अंतरिम समझौते से हमारे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। वे बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकेंगे। मेरा मानना है कि भारतीय निर्यातक अपने प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला कर पाएंगे, क्रिसमस के दौरान छूटी आपूर्ति श्रृंखलाओं को फिर से सक्रिय कर सकेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय निर्यात न केवल बढ़े बल्कि आने वाले वर्षों में भी अच्छा प्रदर्शन करे।’’
कपड़ा, परिधान, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्र अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत के भारी शुल्क से प्रभावित हुए थे। अमेरिकी प्रशासन ने 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क हटा दिया है और जवाबी शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया है।
अग्रवाल ने साथ ही कहा कि हितधारक एवं निर्यातक इस परिणाम से खुश हैं और उन्होंने समग्र समझौते पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा, ‘‘ अंतरिम समझौते में हमने जो हासिल किया है, वह भारत और हमारे निर्यात के लिए अच्छा है। मुझे इसमें कोई बड़ी खामी नजर नहीं आती।’’ (भाषा)