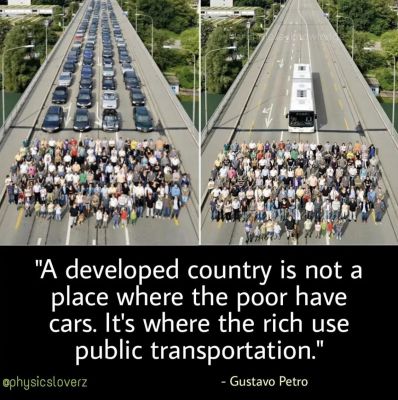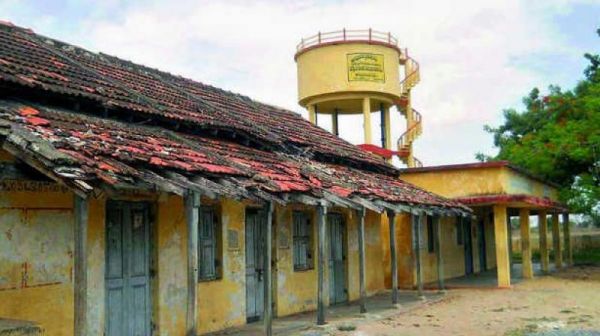संपादकीय
भारत में इन दिनों चल रहा पूर्ण कुम्भ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जलसा है। इस मेले में दसियों करोड़ लोगों के पहुंचने का आसार है, और हिन्दू मान्यताओं के मुताबिक इस बार का कुम्भ 144 बरस में एक बार होता है, इसलिए भी केन्द्र और राज्य सरकार ने इस धार्मिक आयोजन पर हर किस्म का खर्च करना तय किया है। यहां दसियों करोड़ लोग पहुंचेंगे, इसलिए कुछ गिने-चुने लोगों के बर्ताव से इसकी सफलता या असफलता, इसके अच्छे या बुरे होने का फैसला नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उनसे कुछ लोगों के चाल-चलन पर तो रौशनी पड़ती ही है। वहां से जितने किस्म के वीडियो निकलकर बाहर आ रहे हैं, वे पूरी तरह गढ़े हुए नहीं हैं, और अब तक ऐसी कोई शिकायतें भी सामने नहीं आई हैं कि लोगों ने कोई नाटक रचकर कुम्भ को बदनाम करने की कोशिश की हो। हर दिन दस-बीस ऐसे नए वीडियो देखने मिल रहे हैं जिनमें साधू दिखने वाले लोग कुम्भ की सार्वजनिक जगहों पर, और लोगों के बीच खुलकर गालियां बक रहे हैं। वे कैमरों के सामने गालियां दे रहे हैं, अपने चिमटे लेकर लोगों को दौड़ाते हुए गालियां दे रहे हैं, किसी मुस्लिम फेरीवाले को कई साधू लात मार-मारकर भगा रहे हैं कि मुस्लिम यहां पर आया कैसे?
अब सवाल यह उठता है कि अपने आपको साधू या संन्यासी कहने और दिखाने वाले लोग जो कि कहने के लिए पारिवारिक और सांसारिक जीवन की मोह माया से मुक्त हो चुके हैं, वे किस तरह नाराज होने पर पल भर में दूसरों की मां-बहन से अपना रिश्ता जोडऩे की गालियां देने लगते हैं? वैराग्य से पल भर में सेक्स तक पहुंच जाने की उनकी जुबान उन्हें क्या साबित करती है? हम यहां पर साधुओं के हुलिए में गांजा पीते दिखने वाले अनगिनत लोगों की बात नहीं करते, क्योंकि हिन्दुस्तान में गांजा चाहे जितना भी गैरकानूनी क्यों न हो, वह अनंतकाल से प्रचलन में रहा है, और हिन्दू धर्म से जुड़े हुए संन्यासी-बैरागी सार्वजनिक जगहों पर, मठ-मंदिर में, और चबूतरों पर खुलेआम गांजा पीते दिखते हैं, और इसे हिन्दू धर्म के रीति-रिवाज का एक हिस्सा मान लिया गया है। वैसे भी हम बीच-बीच में यह सवाल उठाते रहते हैं कि क्या शराब के अतिसंगठित कारोबार की पकड़ और जकड़ से बाहर निकलकर सरकार को गांजे जैसे कम नुकसानदेह और सस्ते नशे को कानूनी नहीं बनाना चाहिए?
खैर, हम कुम्भ की चर्चा को गांजे तक केन्द्रित रखना नहीं चाहते हैं क्योंकि यह ऐतिहासिक मौका ऐसे किसी एक मुद्दे के मुकाबले बहुत अधिक बड़ा है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यूपी की भाजपा सरकार के हिन्दुत्व के एजेंडे से परे उत्तरप्रदेश ने कुम्भ का इस्तेमाल दुनिया भर से एक धार्मिक पर्यटन को जुटाने में भी किया है। कुछ अरसा पहले यूपी के अयोध्या में शुरू हुए राम मंदिर ने प्रदेश को करोड़ों नए पर्यटक दिए हैं, और कुम्भ दसियों करोड़ नए पर्यटक दे रहा है। यह बात तो समझना बड़ा आसान है कि अयोध्या या कुम्भ जाने वाले धर्मालु पर्यटक या सैलानी इन जगहों से परे भी कुछ दूसरी जगहों पर जाते होंगे, राज्य के बने हुए बहुत किस्म के सामान खरीदते होंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को एकदम से छलांग लगाकर आगे बढऩे में मदद मिलेगी, मिल रही है। उत्तरप्रदेश सरकार अपने राजनीतिक और धार्मिक मकसद में बहुत हद तक कामयाब रही है कि बिना किसी बहुत बड़े हादसे के अब तक दस करोड़ या उससे अधिक लोग वहां आकर लौट चुके हैं।
ऐसे में सरकार के इंतजाम में तो लोगों को बदनामी नहीं दिलाई, जिन लोगों को कुम्भ में स्वाभाविक भागीदार माना जाता है, वैसे भगवाधारी कुछ लोगों ने वीडियो बनाने वाले लोगों की मौजूदगी में जैसी गंदी जुबान इस्तेमाल की है, जैसी साम्प्रदायिकता दिखाई है, उससे वैराग्य के पाखंड का भांडाफोड़ होता है। आज भगवा पहने किसी को भी इस देश में साधू-संन्यासी मान लिया जाता है, और उसे बाबा कहना शुरू कर दिया जाता है। उनके मुंह से जब मां-बहन की गालियां झड़ते वीडियो रिकॉर्ड होते हैं, तो समझ पड़ता है कि इनकी दाढ़ी-मूंछ, भगवा और भभूत, रूद्राक्ष और चिमटा-कमंडल के पीछे इनकी वही आदिम हिंसा कायम है, और जरा सा मौका मिलते ही वह भभूत चीरकर सतह पर आ जाती है। इसलिए किसी भी कुम्भ के मुकाबले इस बार वीडियो-कैमरे कुछ अधिक हैं, अधिक यूट्यूब चैनल हैं, और सोशल मीडिया पर बनने और फैलने वाली रील्स भी एक नई पेशकश है। इसलिए हो सकता है कि हमेशा से साधू-संन्यासियों के चोले में कई ऐसे लोग रहते आए हों, लेकिन अब वे वीडियो पर अधिक कैद हो रहे हैं, और उनके वीडियो अधिक फैल रहे हैं। यह एक किस्म से अच्छी बात इसलिए है कि लोगों की पोशाक से उनके बारे में धारणा बनाई जाती है, वह इससे टूट रही है, और सकारात्मक या नकारात्मक, किसी भी तरह के मजबूत पूर्वाग्रह रहने भी नहीं चाहिए।
फिलहाल एक सामान्य सी जिज्ञासा यह पैदा होती है कि प्रचलित धारणा के मुताबिक अगर कुम्भ के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने से लोगों के पाप धुल जाते हैं, तो फिर संगम में तो अब पानी बचना ही नहीं चाहिए था, पाप ही पाप रह जाना था, और बाद में वहां पहुंचने वाले लोगों को सिर्फ पाप में ही डुबकी लगाना नसीब होना था। लेकिन धर्म पापमुक्ति को जितनी आसान बताता है, वह उतनी आसान रहती नहीं है। इसलिए किसी डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे ऐसी सोच लोगों को आगे पाप करने का एक हौसला दे सकती है, कुम्भ जैसे आयोजनों के साथ जुड़ी ऐसी जनमान्यताओं से उबरने की भी जरूरत है। तमाम धर्मों में ऐसी मान्यताएं बुरा काम करने वाले लोगों को आत्मा धोने की सहूलियत देती हैं, लेकिन समझदारों को कुम्भ के ऐसे किसी संभावित इस्तेमाल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दुनिया का कोई भी धर्म ऐसी कोई भी सी सहूलियत नहीं दे सकता, और धर्म के नाम पर कारोबार करने वाले लोग जरूर ऐसा झांसा बनाए रखते हैं। इसलिए कुम्भ जाने वाले लोग धार्मिक आस्था से जरूर जाएं, या सैलानी की जिज्ञासा से पहुंचें, लेकिन एक डुबकी से पापमुक्ति जैसे झांसे में न आएं, अपने कर्म ही ठीकठाक रखें।
मध्यप्रदेश में सरकारी अफसरों का रूख वहां के मंत्रियों का चेहरा देख-देखकर तय होता है, और लोकतंत्र में सरकार का बहुत सारा काम तो अफसरों के रूख के मुताबिक ही होता है, या नहीं होता है। अब जैसे सरकार का रूख कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ है, तो कांग्रेस के किसी कार्यक्रम के लिए दी गई इजाजत भी उसी हिसाब से ढल जाती है। इंदौर जिले में कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी की आमसभा के लिए सरकारी कॉलेज के मैदान को मांगा, और लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत भी। इस पर एसडीएम की तरफ से जो अनुमति दी गई है, उसमें एक बड़ी दिलचस्प शर्त दिख रही है, कि कार्यक्रम के समय घोषणा करने के दौरान कोई भी राजनैतिक व धर्मविरोधी भाषण प्रतिबंधित रहेंगे। राहुल गांधी सांसद हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, और देश के एक प्रमुख नेता हैं। अब अगर उनके कार्यक्रम की इजाजत में राजनीतिक भाषण प्रतिबंधित रखा जाएगा, तो वे भाषण क्या देंगे? क्या संसद में किसी को बोलने की इजाजत देने के पहले यह कहा जा सकता है कि वे देश के मुद्दों पर नहीं बोलेंगे?
इस मध्यप्रदेश का एक दूसरा आदेश इसी के टक्कर का है। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने अडानी कंपनी के लिए किए जा रहे जमीन अधिग्रहण को लेकर एक आदेश निकाला है जिसमें जिला दंडाधिकारी की हैसियत से हुक्म दिया गया है- जिला छिंदवाड़ा की तहसील हर्रई की समस्त राजस्व सीमाओं में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वॉट्सऐप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से बांध निर्माण से संबंधित संदेश/वीडियो पोस्ट किया जाना अथवा भ्रामक खबरें प्रसारित करना प्रतिबंधित किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कलेक्टर ने इस आदेश को आम जनता को संबोधित रखा है, और लिखा है- चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है, और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए, इसलिए यह एकपक्षीय पारित किया जाता है। यह बांध सर्वे कार्य से लेकर बांध निर्माण कार्य संपन्न होने तक की अवधि तक लागू रहेगा।
ये दोनों आदेश मध्यप्रदेश सरकार के राजनीतिक रूख को बताते हैं। एक आदेश में राहुल की सभा में राजनीतिक बात न होने का हुक्म दिया गया है, तो दूसरे में अडानी के बांध के लिए जमीन अधिग्रहण के पहले से लेकर बांध निर्माण कार्य संपन्न होने तक के लिए पूरी तहसील में किसी भी तरह के मैसेज या वीडियो पर इस बारे में कुछ कहने पर रोक लगाई गई है। कलेक्टर ने इस तहसील के हर नागरिक के गले में एक-एक फंदा डालकर उसे इतना टाईट कर दिया है कि अडानी के खिलाफ कोई आवाज न निकले, बस सांस लेने जितनी जगह बनी रहे। हमारी याद में यह हिन्दुस्तान का अकेला ऐसा गला घोंटने वाला आदेश होगा जो कि भूमि अधिग्रहण के पहले से लागू हुआ है, और बांध निर्माण पूरा हो जाने तक लागू रहेगा! क्या यह किसी किस्म का लोकतंत्र कहा जा सकता है? कोई कंपनी, कोई उद्योगपति सरकार के चहेते हो सकते हैं, लेकिन क्या उनकी गुलामी करने में सरकार लोकतंत्र का ही गला घोंट दे? आज जिस वक्त हम यह संपादकीय लिख रहे हैं, उसी वक्त एमपी में कांग्रेस पार्टी ‘जय बापू, जय भीम, जय संविधान’ नाम का राष्ट्रीय कार्यक्रम डॉ.भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि, महू में शुरू कर रही है। पूरी पार्टी यहां मौजूद रहेगी, और कांग्रेस ने यहां एक लाख लोगों के इकट्ठा होने का अनुमान लगाया है। 2023 में विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस का इस प्रदेश में यह पहला बड़ा कार्यक्रम है, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस कार्य समिति के सारे सदस्य इसमें रहेंगे, और मंच से कोई भी राजनीतिक भाषण होने पर यह अनुमति खुद ही निरस्त हो जाएगी!
सरकारी अफसरों को किसी पार्टी के कार्यकर्ता, या इंडस्ट्री के मुलाजिम की तरह काम करने के पहले यह भी सोच लेना चाहिए कि वे इन बातों के लिए किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तलब भी किए जा सकते हैं। लेकिन अकेले इसी प्रदेश के ऐसे दो अफसर यह कर रहे हों, ऐसा भी नहीं है। बहुत से प्रदेशों में अतिउत्साही अधिकारी, अपनी न जाने किस किस्म की आत्मरक्षा के लिए खुशामदखोर होकर जनविरोधी काम करने लगते हैं, और प्रजा को दुलत्ती मारकर सत्ता की चापलूसी करने लगते हैं। अब अडानी का बांध अगर बीस बरस में बनेगा, तो इन बीस बरसों में भी उस तहसील के लोगों को बांधी की जमीन से लेकर बांध निर्माण तक कुछ कहने का कोई हक नहीं रहेगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटने का ऐसा भयानक काम शायद ही कहीं और याद पड़ता हो। इस आदेश को देखकर वैसे तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की पुरानी इमारत, और संसद की नई इमारत, इन दोनों के मुंह से आह के साथ यह निकलना था कि हे धरती तू फट जा, और हमें समा ले।
लेकिन हमारा ख्याल है कि न सिर्फ ये दो अफसर, बल्कि इनकी ‘जात’ के इनके सरीखे बाकी अफसर भी किसी अदालती धिक्कार को सत्ता के प्रति अपनी निष्ठा के सुबूत की तरह सीने पर टांगकर घूमेंगे, और शहादत के अंदाज में सत्ता को यह समझाएंगे कि उसके लिए वे किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए एक पैर पर खड़े हैं। उनका बस चलेगा तो अपने ऐसे आदेशों के लिए वे महीना-पन्द्रह दिन जेल भी काट आएंगे, और उसे भी अपने गोपनीय प्रतिवेदन में उपलब्धियों के कॉलम में दर्ज करवाएंगे। जब भारतीय लोकतंत्र में नीचे से ऊपर तक सत्ता पर बैठे हुए लोग संविधान की हेठी करने में जुटे हुए हों, तब किसी गरीब या कमजोर के लिए इंसाफ पाने की गुंजाइश न के बराबर रह जाती है, खासकर तब जब वह किसी ताकतवर के जुल्म के सामने कमजोर को इंसाफ मिलने की हो। अब भला एक तहसील की जनता का क्या हक बनता है कि वे अडानी के किसी बांध के बारे में मुंह भी खोलें! ऐसे तमाम मुंह कलेक्टर के आदेश वाले पन्नों से ठूंस-ठूंसकर भर दिए जाएंगे, और कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि जब बांध पूरा हो जाएगा, उसके बाद मुंह में ठूंसे कागज निकाले भी जा सकेंगे। सोशल मीडिया पर कुछ अरसा पहले, देख रहा है बिनोद, यह लाईन बड़ी चली थी। हम सोच रहे हैं कि, देख रहा है सुप्रीम कोर्ट, यह लाईन भी चलनी चाहिए, और उससे हो सकता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत को भविष्य के इतिहास में दर्ज होने वाले अपने नाम की थोड़ी-बहुत फिक्र होने लगे।
कल की दो घटनाएं यह सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि समाज में पैसों की ताकत इतनी बढ़ गई है कि कानून और सरकार भी बेबस हो गए हैं। भिलाई के एक रिहायशी अहाते में एक कार से पहुंचे आधा दर्जन रईसजादों से जब गार्ड ने रजिस्टर पर नाम लिखने कहा तो उन्होंने कार से उसे कुचल डाला। एक दूसरा वीडियो सामने आया है जिसमें किसी और जगह छत्तीसगढ़ में ही कुछ दूसरे रईसजादे एक कार दौड़ाते हुए शहरी इलाके में घूम रही बाघिन का पीछा कर रहे हैं, बुरी तरह से रात में कार की रौशनी में उसे दौड़ा रहे हैं, और जब कार बहुत पास पहुंच जाती है, तो उसे कूदकर एक दीवार पर चढऩा पड़ता है, और उसे समझ नहीं पड़ रहा है, दूसरी तरफ कार से पीछा करते हुए भी जो लोग वीडियो बना रहे थे, वे कार से निकलकर कूद-कूदकर तस्वीरें खींच रहे हैं, और वीडियो बना रहे हैं। और राष्ट्रीय पशु को यह समझ नहीं पड़ रहा है कि वह क्या करे?
भिलाई में गार्ड को जिन लोगों ने कुचला, वे, कम से कम गाड़ी चलाने वाला एक व्यक्ति किसी ट्रांसपोर्टर परिवार का बताया जा रहा है। ऐसे में साथ में घूम रहे युवक-युवतियों की बददिमागी का अंदाज लगाया जा सकता है। हम अलग-अलग शहरों में आए दिन इस तरह के वीडियो देखते हैं जब देर रात तक गैरकानूनी तरीके से चलते हुए शराबखानों से निकलते पैसेवाले लडक़े-लड़कियों की किसी और टोली से मारपीट होती है, और पुलिस और प्रशासन का मानो वहां कोई असर ही नहीं रहता। तमाम सडक़ों पर यह देखने में आता है कि जितनी बड़ी गाड़ी में लोग चलते हैं, उनकी बददिमागी उसी अनुपात में रहती है। इंसान की ताकत के साथ मानो गाड़ी का हॉर्सपॉवर जुडक़र उन्हें और अहंकारी बना देता है। ऐसे ही लोग बड़ी-बड़ी गाडिय़ों में आड़ी-तिरछी नंबर प्लेट लगवाते हैं, ऊपर बड़ी-बड़ी लाईटें लगवाते हैं, सायरन और हूटर लगवाते हैं, और अंधाधुंध रफ्तार से गाडिय़ों को दौड़ाते हैं। सार्वजनिक जीवन में ऐसा लगता है कि ओहदे और दौलत की जितनी ताकत जिसके पास है, उसके उतने ही अधिक विशेषाधिकार इस लोकतंत्र में हो गए हैं। ऐसे लोग दारू या दूसरे किस्म के नशे में दूसरों को कुचलने के लिए तैयार रहते हैं, और साथ-साथ अपने से कमजोर लोगों को भुनगों जैसा समझते हैं, जैसा कि कल भिलाई में एक कॉलोनी के गार्ड को समझ लिया गया, उसे सबक सिखाने के लिए गाड़ी से कुचल दिया गया, और आज अभी कुछ मिनट पहले उसके वेंटिलेटर पर रहने की खबर भी है, और मर जाने की भी।
दरअसल ओहदे और दौलत की ताकत इतनी अधिक रहती है कि सत्ता चलाने वाले नेता उन्हें साथ रखना पसंद करते हैं। ऐसे में छोटे अफसरों का यह हौसला भी नहीं रहता कि ताकतवर लोगों पर हाथ डालें। आज भी पुलिस तक जब किसी गुंडागर्दी या अराजकता की शिकायत पहुंचती है, तो जुर्म की गंभीरता आंकने से पहले पुलिस यह देखती है कि जुर्म की तोहमत किस पर लग रही है। अगर यह सिर्फ पैसों की ताकत वाले पर है, तो पुलिस के बहुत से लोग ऐसे मुजरिम परिवार को दुधारू गाय मानकर चलते हैं। अगर यह तोहमत किसी राजनीतिक ताकत वाले के खिलाफ रहती है, तो पुलिस का रूख यह रहता है कि मामला कैसे-कैसे नहीं बने। यह सिलसिला आम जनता को आम भी नहीं, गुठली मानकर चलता है, और आज अधिकतर मामलों में कोई कार्रवाई तभी होती है जब मुजरिम ताकतवर न हो, या उसके खिलाफ पुख्ता वीडियो-सुबूत हों जिन्हें नकार पाना आसान न हो। यह व्यवस्था समाज में पैसे और ताकत की वजह से छाई हुई एक गैरबराबरी का खतरा बताती है जिसमें गरीब और कमजोर के किसी भी तरह का इंसाफ पाने की कोई गुंजाइश नहीं रहती।
कोई भी देश-प्रदेश अगर जुर्म कम करना चाहते हैं, तो उन्हें ताकतवर तबके की बददिमागी से उपजे हुए जुर्म पर रोक लगानी ही होगी। ताकत से चाहे अफसरों पर खतरा पैदा होता हो, या उनसे कमाई की गुंजाइश हो, अगर ताकत की बददिमागी को बिना सजा जारी रखने दिया जाएगा, तो वह और लोगों पर भी निकलेगी। आज वह एक कॉलोनी के गार्ड को कुचल रही है, कल वह किसी पुलिस वाले को कुचलेगी, और इसके बाद अधिक ताकतवर लोग कम ताकतवर लोगों को कुचलेंगे। आज भी सडक़ों पर जिस तरह का आतंक ताकतवर लोग दिखाते हैं, उनकी बिगड़ैल औलादें दिखाती हैं, वह बहुत ही खतरनाक नजारा रहता है। लोग अपनी बड़ी गाड़ी की ताकत से दूसरे लोगों से यह सहज सवाल करते हैं- जानता नहीं मेरा बाप कौन है?
ताकत की ऐसी गुंंडागर्दी पर रोक लगाने के लिए सत्ता में एक इंसाफ की समझ जरूरी होती है, और लोगों को बराबर मानकर चलने के लोकतांत्रिक मूल्य भी जरूरी होते हैं। इसके बिना ऐसे देश-प्रदेश पूरी तरह से असभ्य होते हैं, और खतरनाक भी होते चलते हैं। हम पहले भी दर्जनों बार इस बात की वकालत कर चुके हैं कि जिस जुर्म के लिए किसी गरीब को दो बरस की कैद होनी है, तो वही जुर्म अगर ताकतवर करे, तो उसे चार बरस की कैद होनी चाहिए, और अगर वह किसी कमजोर के खिलाफ करे तो छह बरस की। जब तक इंसाफ इस किस्म के एक अनुपात को लेकर नहीं चलेगा, तब तक असमानता से भरापूरा हिन्दुस्तान जैसा लोकतंत्र सबसे कमजोर को कभी इंसाफ नहीं दे सकेगा। पुलिस, गवाह, सुबूत, वकील, और अदालतें, इन तमाम जगहों पर पैसा सिर चढक़र बोलता है, और गरीब या कमजोर के खिलाफ ये तमाम ताकतें लग जाती हैं। इसलिए समाज के लोगों को भी सत्ता पर यह दबाव बनाकर रखना चाहिए कि ताकत की हिंसा को खत्म किया जाए। आमतौर पर ताकत की हिंसा के सुबूत खत्म किए जाते हैं, ताकि ताकत पर आंच न आए।
हर दिन के अखबार ऐसी खबरों से पटे रहते हैं कि जिसकी जो सरकारी जिम्मेदारी रहे, उसके ठीक खिलाफ जाकर लोग जुर्म करते दिखते हैं। आज ही की कुछ खबरों को लें, तो लोगों को ठगने के लिए, ठगी का पैसा कुछ फर्जी बैंक खातों में डालकर उसे कहीं और पहुंचा देने के लिए इस्तेमाल हो रहे सैकड़ों बैंक खाते पकड़ाए हैं, और इनमें बैंक अफसरों की मिलीभगत (वैसे मिलीमौलाना, या मिलीपादरी कहना चाहिए क्या?) सामने आई है। जिन लोगों को बैंक के काम के लिए तनख्वाह मिलती है, वे बैंक को लुटेरों के हाथ बेच रहे हैं। कल ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की एक सडक़ का वीडियो सामने आया जिसमें बिना वर्दी के एक पुलिस अधिकारी सडक़ के बीच मोटरसाइकिल का यूटर्न ले रहा है, और पीछे से आ रही एक दुपहिया आकर उससे टकरा जाती है। दुपहिया चला रही महिला को यह पुलिसवाला घूंसे मारता है, और गालियां देता है, इसके बाद वहां से चले जाता है। जिस पुलिस के जिम्मे कानून व्यवस्था रहती है, वह इस किस्म की असभ्य और गैरकानूनी हरकत करता है। एक और खबर बताती है कि टोल टैक्स नाके पर सरकार और नाका ठेकेदार के लिए नगद वसूली सॉफ्टवेयर बनाने वाला उसमें ऐसी गड़बड़ी करता है कि नगद वसूली की फर्जी रसीद निकलती है, और सरकार का हिस्सा उसे जाता ही नहीं, पूरा पैसा टोल नाका ठेकेदार कंपनी को चले जाता है, और यह धोखाधड़ी सौ करोड़ से अधिक की हुई है। जिस सॉफ्टवेयर बनाने वाले को सरकारी टैक्स की हिफाजत का ध्यान रखना था, उसने धोखाधड़ी और जालसाजी का पुख्ता इंतजाम रखा। ऐसे मामले हर दिन सामने आते हैं जिनमें दिखता है कि बाड़ ही खेत खाने लगी है, किसी बाहरी की जरूरत नहीं रह गई है। ऐसे लोगों का क्या किया जाना चाहिए?
जब दुश्मन घर के भीतर हो, जब चौकीदार ही चोर बन जाए, जब जनता के पैसों पर पलने वाले अधिकारी-कर्मचारी जनता के हक के साथ धोखाधड़ी, और जालसाजी करने लगें, तो क्या ऐसे लोगों को सजा देने के लिए अलग से कुछ कानून नहीं बनना चाहिए? क्या मौजूदा कानून में और अधिक कड़ाई नहीं बरतना चाहिए? क्या ऐसे लोगों की जमीन-जायदाद को जब्त करके सरकार को लगाए गए चूने की रिकवरी नहीं करनी चाहिए? ऐसे बहुत से सवाल इस देश में रोजाना हो रहे जुर्म को लेकर उठते हैं। कहीं राह चलता कोई आदमी किसी महिला से बलात्कार करे, तो उस पर जितनी सजा का इंतजाम हो, उससे कई गुना अधिक सजा ऐसे लोगों को होनी चाहिए जो कि शिक्षक होते अपनी छात्राओं से ऐसा करें, या खेल प्रशिक्षक होते हुए अपनी खिलाड़ी के साथ ऐसा करें। जिन लोगों के हवाले सरकारी कामकाज और उनसे जुड़े हुए अधिकार रहते हैं, उनके किए हुए जुर्म अधिक सजा के हकदार रहने चाहिए।
भारत में पता नहीं कैसे लोगों के मन में इस किस्म के जुर्म के लिए खौफ एकदम ही खत्म हो गया है। कहने के लिए तो देश की आबादी का तकरीबन पूरा ही हिस्सा अपने को धर्मालु मानता है, तरह-तरह के धार्मिक पाखंड भी करता है, नैतिकता की बातें कहने वाले प्रवचनकर्ताओं को सुनने के लिए घंटों बैठता भी है, धार्मिक प्रतीक पहनता है, पापमुक्ति के हर किस्म के औजारों का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन फिर अपनी हर किस्म की ताकत को हथियार की तरह इस्तेमाल करके जुर्म भी करता है। धर्म और जुर्म का यह तालमेल गजब की संगत दिखाता है। जिस तरह संगीत में दो अलग-अलग वाद्ययंत्रों के बीच जुगलबंदी होती है, ऐसे ही हिन्दुस्तान में (और बाकी दुनिया में भी) जुर्म और धर्म की जुगलबंदी देखने लायक रहती है। गॉड फादर जैसी फिल्म देखें, तो माफिया सरगना धार्मिक भावना से लबालब दिखते हैं, चर्च जाते हैं, अपने ही किए हुए कत्ल की लाश के कफन-दफन के वक्त धार्मिक संस्कार के लिए मौजूद रहते हैं, और ईसा मसीह को याद करते हैं। छत्तीसगढ़ में दो दिन पहले एक ही दिन में दो अलग-अलग जगहों पर दो पतियों ने अपनी-अपनी पत्नियों को मार डाला, दोनों पतियों के नाम में राम का नाम था, और उनके पिताओं के नाम में भी राम का नाम था। राम के नाम ने किसी भी जुर्म से नहीं रोका। इसी तरह सरकारी नौकरी के नियम किसी को भ्रष्टाचार से नहीं रोक रहे, और रिश्वत जैसे जुर्म से बहुत आगे बढक़र जो लोग धोखाधड़ी और जालसाजी के दर्जे की साजिश तैयार करते हैं, उनके मन में भी न सरकारी नियमों का खौफ रहता, न अदालती सजा का, और न ही अपने धर्म का। बल्कि धर्म तो अधिकतर मामलों में लोगों को पाप और बुरे काम करने का हौसला देता है क्योंकि वह पापमुक्ति से लेकर प्रायश्चित तक के लिए तरह-तरह के इलाज और समाधान सुझाता है। कहीं गंगा में डुबकी लगाई जा सकती है, कहीं चर्चा में जाकर कन्फेशन चेम्बर में अपराध माना जा सकता है, और कहीं मस्तान भी हाजी बनकर जुर्म जारी रख सकता है। तकरीबन तमाम धर्म ऐसी लॉंड्री सेवा मुहैया कराते हैं। इसलिए किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी से किसी धार्मिक सीख या नसीहत की वजह से बेहतर इंसान बनने की उम्मीद नहीं की जा सकती, और कानूनी बंदिशों को तोड़ते हुए जुर्म करने, और बच जाने की सहूलियतों पर लोगों का अपार भरोसा भी है।
ऐसे में समाज और सरकार दोनों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि मुजरिम और पापी के लिए कुछ खास इंतजाम किया जाए। सरकार तो सिर्फ जुर्म पर सजा दे सकती है, लेकिन धर्म के ठेकेदार पापियों के लिए भी कुछ रोक-टोक तय कर सकते हैं। बहुत से मामलों में इन दोनों की जरूरत है। कानून अपना काम करे, और धर्म अपना। हम रोज ही सडक़ों पर ऐसे बहुत से लोगों को नियम-कानून तोड़ते, और जुर्म करते देखते हैं जो कि अपनी गाडिय़ों पर धर्म के निशान लगाकर चलते हैं, धार्मिक नारे लिखवाकर चलते हैं, या अपने बदन पर धार्मिक प्रतीक पहने रहते हैं। जाहिर है कि उनके हर गलत काम से उनके धर्म की भी बदनामी होती है, और देश-प्रदेश के कानून तो टूटते ही हैं। धर्म के ठेकेदारों को भी अपने लोगों के गलत काम और जुर्म पर सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए, और उन पर सार्वजनिक रोकटोक भी लगानी चाहिए। किसी धर्म और उसके ईश्वर का सम्मान भला कहां बच जाता है जब पुख्ता साबित हो चुके मुजरिमों के लिए भी उनके दरवाजे खुले रहते हैं? जिस तरह किसी भ्रष्ट को सरकारी सेवा से निकालने का कानून है, उसी तरह बुरे मुजरिमों को धर्म से बाहर करने का भी एक रिवाज होना चाहिए। इटैलियन माफिया के बारे में पोप सोच लें, इस्लामी आतंकी हत्यारों के बारे में कोई इमाम सोच ले, और पत्नी को मारकर टुकड़े करके कुकर में पकाने वाले हिन्दू के बारे में शंकराचार्य सोच ले, क्योंकि ये लोग सेवा नियमों से बंधे हुए सरकारी कर्मचारी तो हैं नहीं, धर्मालु मुजरिम जरूर हैं। सरकार और समाज दोनों ही अपने-अपने पैमाने कड़ाई से लागू न कर पाएं, तो फिर उनकी सत्ता ही क्या है, क्या ख्याल है? (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
चारों तरफ से आती खबरों में दो किस्म की खबरें सबसे ऊपर दिखती हैं, एक तो तरह-तरह की उम्र के लोग खुदकुशी कर रहे हैं। इनमें गरीब भी हैं, मध्यवर्गीय भी हैं, और संपन्न लोग भी हैं। दूसरी तरफ हर दिन ही अनगिनत मामले ऐसे वैध-अवैध संबंधों के आ रहे हैं जिनमें लडक़े-लडक़ी के बीच देहसंबंध बने, और फिर शादी का वायदा करके शादी न करने जैसी शिकायत हो गई, और फिर कुछ मामलों में बलात्कार का मामला दर्ज करवाया गया, और कुछ दूसरे मामलों में देहसंबंधों के दिनों में बनाए गए वीडियो दिखा-दिखाकर बलात्कार जारी रखा गया, या फिर ब्लैकमेल किया गया, और देहसंबंधियों के बीच मरने या मारने की नौबत आ गई। कई मामलों में तो प्रेमी-प्रेमिका, और पति के बीच किसी ने किसी को मार डाला, और फिर खुदकुशी कर ली। इन तमाम किस्म की निजी हिंसाओं की वजहों का कोई विश्लेषण किया जा सकता है?
गरीब के बच्चों को मां-बाप के संघर्ष पर रहम नहीं आती, उन्हें स्मार्टफोन पाने की अपनी हसरत इतनी महत्वपूर्ण लगती है कि वह फरमाईश पूरी न होने पर उन्हें खुदकुशी करने में वक्त नहीं लगता। कुछ बच्चे मां-बाप के पैसे चुराकर भी मोबाइल फोन या इस किस्म की दूसरी हसरतें पूरी करते हैं। लेकिन उन गरीब मां-बाप की दिमागी हालत के बारे में सोचा जाए कि स्मार्टफोन न दिला पाने पर बेटे या बेटी ने खुदकुशी कर ली, और उसके बाद वे पूरी जिंदगी इस मलाल में जीते रहेंगे कि कर्ज लेकर भी अगर फोन दिला दिया रहता तो भी बच्चे तो जिंदा रहते। ऐसे दुख में डूबे मां-बाप यह भी नहीं सोच पाते कि फरमाईश फोन पर नहीं थमती, वह फोन के बाद किसी बाइक पर आ जाती, और फिर तब तक फोन का अगला मॉडल आ जाता, और कुछ बरस बाद बाइक का नया मॉडल आ जाता, और इस बीच फोन के री-चार्ज और बाइक के फ्यूल टैंक का खर्च जुड़ा ही रहता। फरमाईशों का कोई अंत नहीं होता। एक-दूसरे के देखादेखी बच्चों और नौजवान पीढ़ी के मन में सामानों की हसरत पैदा होती रहती है, और एक-दूसरे से पिछड़ न जाने के दबाव में वे जायज या नाजायज तरीकों से सामान हासिल करने में लगे रहते हैं, और ऐसे में ही कई बार नाबालिग बच्चे सामानों के मोह में बालिग लोगों के साथ देहसंबंधों में उलझ जाते हैं। इनके बीच मोहब्बत शायद कम मामलों में रहती होगी, अपनी हसरत पूरी होने की हसरत अधिक रहती होगी। कुल मिलाकर लोग संघर्ष की जिंदगी के रास्ते अपनी चाहत पूरी करने, सामान और सहूलियत हासिल करने पर कम भरोसा करते हैं, वे एक ऐसा शॉर्टकट ढूंढते हैं जिससे रातों-रात उन्हें सब कुछ हासिल हो जाए। इसी चक्कर में बहुत सी लड़कियां और महिलाएं सेक्स, वीडियो, बलात्कार, ब्लैकमेल जैसी अंधेरी और अंतहीन सुरंग में फंस जाते हैं। नतीजा यह होता है कि लोग खुदकुशी करते हैं, या ब्लैकमेल करने वाले को मार भी डालते हैं।
आज बाजार जिस हमलावर तेवरों के साथ इंसानों को ग्राहक बनाने पर आमादा है, और हर इंसान अपनी ताकत और औकात से आगे बढक़र अधिक से अधिक बड़े और खर्चीले ग्राहक बनने पर आमादा हैं, उसे देखकर हैरानी होती है कि क्या इंसान महज ग्राहक बनकर ही खुश हैं? क्या उनकी जिंदगी का अकेला मकसद महज ग्राहक बन जाना है? क्या मेहनत और कामयाबी पाए बिना महज सामानों के मालिक होने की शोहरत, दिखावे की चमक-दमक, और उससे लोगों की नजरों में महत्व पाने की चाहत ही सब कुछ रह गई है? क्या जिंदगी के बाकी मूल्य कुछ भी नहीं रह गए हैं? क्या अपने ही परिवार के बड़े लोगों की संघर्ष की जिंदगी और मेहनत की मिसाल कुछ नहीं रह गई है? यह पूरा सिलसिला इतना निराश करता है कि इंसान महज एक ग्राहक और उपभोक्ता की शक्ल में संतुष्ट और खुश हैं, उन्हें बेहतर इंसान बनने की कोई हसरत नहीं है, और जिंदगी की असल कामयाबी पाने की मेहनत करने की उनकी नीयत नहीं है।
आज मध्यमवर्गीय और गरीब परिवार ऐसी दिक्कतों को सबसे अधिक झेल रहे हैं। जो संपन्न परिवार हैं वे अपने बच्चों को लाख रूपए के मोबाइल, और लाखों रूपए की बाइक लेकर देने की हालत में रहते हैं। वे अपने बच्चों को क्रेडिट कार्ड भी दे देते हैं। लेकिन समाज इतना मिलाजुला है कि ऐसे हर संपन्न बच्चे के इर्द-गिर्द उससे बहुत कम संपन्न बच्चे भी रहते हैं, और उनके सामने संपन्नता का यह वैभव प्रदर्शन चलते रहता है, जिससे उनकी आंखें चकाचौंध रहती हैं। अब आए दिन लोगों के इस्तेमाल होने वाले कपड़े, जूते, फिटनेस बैंड, ब्लूटूथ जैसे दर्जनों सामान रहते हैं जो कि सबसे संपन्न के पास आते-जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और जिन्हें देख-देखकर उनसे कम संपन्न लोग लगातार एक कुंठा में जीते हैं। उनकी अपूरित हसरतें उन्हें अपने ही मां-बाप के खिलाफ बागी बना देती हैं जो कि ऐसे महंगे इंतजाम नहीं कर पाते। भ्रष्ट नेता-अफसर-ठेकेदार की औलादें अपने ईमानदार मां-बाप, या गरीब मां-बाप पर तरस खाती हैं कि न वे कमाना सीख पाए, न अपने बच्चों को ‘अच्छी’ जिंदगी दे पाए। यह सिलसिला स्कूल से कॉलेज तक, और कॉलेज के बाद भी नौजवानों के यारी-दोस्ती, और प्रेमसंबंध के दिनों तक चलते रहता है, भड़ास बढ़ती रहती है, और जाने कब इन चीजों की चाहत में नाबालिग देहसंबंध में फंस जाते हैं, और बालिग लड़कियां या महिलाएं अवांछित संबंधों में, जिनका अंत ब्लैकमेलिंग और हिंसा तक पहुंच जाता है।
हम यहां किसी प्रवचनकर्ता की तरह नैतिकता की नसीहतें देना नहीं चाहते, क्योंकि उनके कोई ग्राहक नहीं रह गए हैं। आज प्रवचन भी सिर्फ धार्मिक, धर्मान्ध, साम्प्रदायिक किस्म के चल पा रहे हैं, इन तीनों विशेषणों से दूर रहने वाले विवेकानंद जैसे व्यक्ति की बातों का भी आज कोई बाजार नहीं है, उन्हें भी सुनने वाले कोई नहीं हैं। लेकिन किया क्या जाए? जैसे-जैसे सरकार और राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ते चल रहा है, समाज में हर किस्म का कारोबार करने वाले लोग कालेधन का सुख पा रहे हैं, वैसे-वैसे समाज में गैरजरूरी फिजलूखर्ची, महंगे सामानों का इस्तेमाल, हिंसक होने की हद तक का दिखावा, तरह-तरह के आडंबर खूब चल रहे हैं, और इनसे दूर रह पाना, इनसे अछूता रह पाना शायद किसी के लिए भी मुमकिन नहीं रह गया है। आज लोग इस्तेमाल के सामान पाकर भी खुश नहीं हैं, जब तक कि उनके साथ ऐसा ब्रांड जुड़ा हुआ न हो जो कि आज की सामाजिक प्रतिष्ठा का एक प्रतीक बन गया है। ऐसा दिखावा खुद के खिलाफ हिंसक बन जाता है, मां-बाप पर हिंसक कर्ज थोप देता है, और ग्राहक कब कई किस्म के मुजरिम बन जाते हैं, यह पता भी नहीं लगता है। बाजार व्यवस्था ने लोगों के सपनों के साथ मिलकर खून से एक ऐसी तस्वीर बना दी है, जिसमें परंपरागत मूल्यों की कोई जगह नहीं है। आज यह सब लिखते हुए हमारे पास समाधान कुछ भी नहीं है, लेकिन हम समस्या को हिंसा की हद तक बढ़ जाने की नौबत लोगों को याद दिला रहे हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
गुजरात के सूरत की तकलीफदेह खबर है कि आठवीं क्लास की एक बच्ची को स्कूल में फीस न दे पाने की वजह से इम्तिहान में नहीं बैठने दिया गया। इसके बाद उसे क्लासरूम के बाहर दो दिन तक शौचालय के करीब खड़ा रखा गया क्योंकि उसके मां-बाप फीस का इंतजाम नहीं कर पाए थे। जब वह घौर लौटी तो बुरी तरह से रो रही थी। पिता ने कहा कि अगले महीने तक फीस का इंतजाम कर लेंगे, लेकिन वह इतनी विचलित थी कि उसने स्कूल जाने से मना कर दिया। और जब मां-बाप काम पर गए हुए थे तो उसने खुदकुशी कर ली। स्कूल ने जाहिर तौर पर आरोपों को गलत बताया है। सरकार ने मामले की जांच का कहा है। अब यह घटना देश के एक सबसे संपन्न और कारोबारी प्रदेश गुजरात की है, जो कि देश के दो सबसे ताकतवर लोगों का गृहराज्य भी है, और जहां पिछले कई कार्यकाल से भाजपा की ही सरकार चली आ रही है। यह नौबत देश में जगह-जगह सामने आती है, लेकिन गुजरात में ऐसा होना अधिक फिक्र की बात है क्योंकि यह देश की सत्ता का अपना गृहराज्य है, और मोदी-शाह की पार्टी भी इस राज्य की सत्ता पर काबिज है।
स्कूली छात्र-छात्राओं को अगर इतने तनाव से गुजरना पड़ता है, तो फिर इस देश को दुनिया के कुछ सभ्य और विकसित देशों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। कल ही छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में एक सरकारी स्कूल की प्राचार्या के खिलाफ अधिक फीस वसूली करने, और शौचालय साफ करवाने के आरोप लगाते हुए छात्र-छात्राओं की बड़ी भीड़ पुलिस को धक्का देते हुए कलेक्ट्रेट में घुस गई, और भारी आक्रोश के नारे लगाने लगी। उसके वीडियो देखें तो लगता है कि तनाव इतना बढऩे के पहले क्या कोई शाला विकास समिति, स्थानीय पार्षद, स्थानीय विधायक या सांसद कोई भी इस तरफ नहीं देखते हैं? कुछ ऐसी ही नौबत प्रदेश में बहुत सी और जगहों पर स्कूलों को लेकर चली आ रही है जहां मास्टर और हेडमास्टर दारू पिए हुए पहुंच रहे हैं, छात्राओं से अश्लील बर्ताव हो रहा है, और कई जगहों पर उनके साथ बलात्कार हो रहा है। कहीं-कहीं आश्रम छात्रावास की बच्चियां गर्भवती हो रही हैं। सरकारी स्कूलों से लेकर महंगी निजी स्कूलों तक सब जगह बच्चों का ऐसा ही बुरा हाल चल रहा है। एक तरफ दिल्ली में केजरीवाल सरकार अपनी स्कूलों के मॉडल तैयार करने के लिए दुनिया में सबसे अच्छी स्कूली पढ़ाई वाले नार्वे से सीख रही है, दूसरी तरफ केरल जैसे राज्य में दक्षिण के बाकी राज्यों से भी आगे बढक़र हर दर्जे की शिक्षा को भरपूर अहमियत दी जा रही है, लेकिन हिन्दीभाषी राज्यों, और उत्तर भारत के राज्यों में पढ़ाई का हाल बहुत ही खराब चल रहा है। खुद भारत सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग की 2023-24 की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि आबादी बढऩे के बाद भी स्कूलों की दर्ज संख्या में 37 लाख से अधिक की गिरावट आई है, और यह गिरावट एसटी-एससी, ओबीसी, और लड़कियों के वर्ग में सबसे अधिक है। आज आई एक दूसरी रिपोर्ट बतलाती है कि पढ़ाई का स्तर किस कदर कमजोर चल रहा है। ऐसे में उन राज्यों को अधिक फिक्र करने की जरूरत है जहां शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, या पश्चिम बंगाल की तरह शिक्षक भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि मंत्री की प्रेमिका का फ्लैट फर्श से छत तक नोटों से भरा मिला था। जब शिक्षक भर्ती का यह हाल रहेगा, तो जाहिर है कि शिक्षा तो बदहाल रहेगी ही। दुनिया के जितने जिम्मेदार देश हैं, उनमें प्राथमिक शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, और बहुत से देश एक-दूसरे के तजुर्बे से सीखते हैं। हिन्दुस्तान में हालत यह है कि पढ़ाई में देश में सबसे आगे जो केरल है, उसी से कुछ सीखने की जरूरत किसी दूसरे प्रदेश को नहीं लगती है। राजनीतिक दलों को लगता है कि दूसरी पार्टी के राज वाले प्रदेश से कुछ कैसे सीखा जाए, और अगर दो राज्यों में सरकार एक पार्टी की ही है, तो भी उन्हें लगता है कि दूसरे प्रदेश को महत्व कैसे दिया जाए। हो सकता है कि दिल्ली को स्कूलें सुधारने के लिए नार्वे जाने की जरूरत न रही हो, और केरल से भी बहुत कुछ सीखा जाना मुमकिन रहा हो, लेकिन राजनीतिक दलों के अपने पूर्वाग्रह, और एक-दूसरे से आगे बढक़र दिखने की चाह सब कुछ रोक देती है।
हम इस नीरस चर्चा को हर कुछ महीने में जरूर छेड़ते हैं क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चों पर ही टिका रहता है। ये बच्चे आज अगर बेहतर न बने, तो इस बात की गारंटी रहती है कि यह देश भी आगे जाकर बेहतर नहीं बन सकेगा। लोकतंत्र में किसी भी देश और प्रदेश को अपने बच्चों को सबसे अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। अभी जापान की स्कूलों की शिक्षा प्रणाली से दुनिया के बिल्कुल दूर कोनों के देश भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। और वहां प्राथमिक शाला में औपचारिक किताबी पढ़ाई के बजाय काम का सम्मान करना, दूसरों के लिए आदर का भाव रखना जैसी बुनियादी बातों को, और कामों को सिखाया जाता है। अब जिस देश-प्रदेश में टीचर क्लास में दारू पिए हुए पड़े रहेंगे, वहां किस तरह की बुनियादी तालीम की बात हो सकती है? भारत के तमाम प्रदेशों को स्कूलों की हालत सुधारने, पढ़ाई का स्तर बेहतर करने, और बच्चों में लोकतंत्र के प्रति सम्मान विकसित करने का काम करना चाहिए, आज की हालत तो बहुत ही निराशाजनक है। इस देश के भीतर भी दक्षिण के राज्य जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, वह देखने लायक है, और वह इसलिए है कि वहां स्कूल-कॉलेज की पढ़ाई को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। उच्च शिक्षा के लिए उत्तर भारत के बच्चे भी दक्षिण की तरफ जाने को मजबूर रहते हैं। नार्वे तो दूर है, दक्षिण से ही कुछ सीख लिया जाए।
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले और लगे हुए ओडिशा राज्य के बीच की सरहद पर कल से चल रही पुलिस-नक्सल मुठभेड़ में अब तक 14 या अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इनमें एक ऐसा नक्सल नेता चलपति शामिल है जिस पर एक करोड़ रूपए का ईनाम था। अभी दो दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक दूसरी मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए थे। कल शाम से चल रही गरियाबंद-ओडिशा सरहद का यह इलाका बस्तर से अलग है। अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद से अब तक मारे गए नक्सलियों की गिनती की जाए तो वह तीन सौ पार दिख रही है। राज्य बनने के बाद से यह पहला ही मौका है जब 13 महीनों में सुरक्षा बलों को नक्सलियों से निपटने में इतनी कामयाबी मिली है। और ऐसे में पांच बरस की पिछली कांग्रेस सरकार से कुछ लोग यह सवाल करना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राज में नक्सल मोर्चे पर इसी पुलिस और इसी पैरामिलिट्री को कामयाबी क्यों नहीं मिल रही थी? और ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस सरकार ने पांच बरस में नक्सलियों से किसी शांतिवार्ता में कामयाबी पाई हो। वैसी न कोई कोशिश हुई, न सुरक्षा बलों को इतनी कामयाबी मिली। चूंकि बस्तर और लगे हुए प्रदेशों में नक्सलियों की वजह से सुरक्षा बलों और ग्रामीणों की भी लगातार मौतें होती हैं, इसलिए यह मुद्दा अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि नक्सलियों से परे भी लोग मारे जाते हैं।
एक पल के लिए कांग्रेस सरकार के आंकड़ों पर नजर डालें, तो उसके आते ही 2019 में 154 नक्सली मारे गए थे, 2020 में 134, 2021 में 128, 2022 में 66, 2023 में 57 नक्सली मारे गए। दूसरी तरफ 2024 में भाजपा सरकार आते ही एक बरस में करीब 300 नक्सली मारे गए, और 2025 के इन पहले तीन हफ्तों में ही 32 नक्सली मारे गए हैं। ये आंकड़े कम से कम सरकार का रूख और रूझान तो बताते ही हैं कि नक्सल मोर्चे पर किसकी क्या नीति थी, और क्या नीति है। हो सकता है कि कोई राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए नक्सलियों से मदद लेते हों, लेकिन आम नागरिकों की, और सुरक्षा बलों की मौत की कीमत पर ऐसी मदद लेना और बदले में रियायत देना तो नाजायज है।
नक्सलियों से बातचीत भाजपा के मुख्यमंत्री रहे डॉ.रमन सिंह ने अपने कार्यकाल में विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह खूब जमकर वजन के साथ की थी, लेकिन वह किसी किनारे नहीं पहुंंच पाई। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शांतिवार्ता की कोई सुगबुगाहट भी पैदा नहीं की, और वे सिर्फ यही कहते रहे कि नक्सली हथियार छोड़ेंगे तो ही उनसे बात होगी। उनका रूख न बातचीत का था, न सुरक्षा बलों की किसी बड़ी और मजबूत कार्रवाई का। भाजपा सरकार आते ही न सिर्फ राज्य के नेताओं ने, बल्कि केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी मार्च 2026 तक नक्सलियों को खत्म करने के इरादे की घोषणा की। अभी जिस रफ्तार से नक्सलियों को खत्म किया जा रहा है, और इक्का-दुक्का मामलों को छोडक़र नक्सलियों के नाम पर बेकसूरों को मार डालने की, फर्जी मुठभेड़ की शिकायतें भी नहीं हैं। तीन सौ नक्सलियों को खत्म करते हुए शायद आधा दर्जन बेकसूर लोगों को मारने के आरोप नक्सलियों ने लगाए हैं, और बाकी सारे लोगों के नक्सली होने की बात खुद उन्होंने ही मान ली है। मानवाधिकार कुचलने, और ज्यादती करने की इतनी कम शिकायतें राज्य बनने के बाद से पहले कभी नहीं रहीं। सुरक्षा बलों के इतने बड़े-बड़े ऑपरेशनों के बाद भी इतनी कम शिकायतें होना सावधान सुरक्षा कार्रवाई का ही संकेत है।
नक्सलियों के हर जत्थे के मारे जाने के बाद उनकी ताकत कमजोर होती जा रही है, और उन पर अगली कार्रवाई कुछ आसान हो रही है। हम केन्द्र सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य और राज्य शासन द्वारा उसे मानी गई चुनौती की तारीख पर कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन नक्सली छत्तीसगढ़ में कमजोर तो बहुत तेजी से हो रहे हैं, और ऐसे में कुछ लोगों को यह भी लग सकता है कि भाजपा के गृहमंत्री विजय शर्मा ने सरकार बनते ही जिस मजबूती से शांतिवार्ता की घोषणा की थी, और उसके बाद किसी वीडियो कॉल पर भी शांतिवार्ता करने के लिए अपना उत्साह दिखाया था, अब उसकी जरूरत नहीं रह गई है। लेकिन हम शांतिवार्ता को बिल्कुल गैरजरूरी मानने के खिलाफ हैं क्योंकि लोगों ने यह भी देखा है कि अभी-अभी बस्तर में 9 सुरक्षा कर्मचारी मारे गए, 24 पिछले बरस मारे गए, और पिछले बरस 80 नागरिक भी मारे गए थे। ये आंकड़े नक्सल मौतों से कम हैं, लेकिन 13 महीनों में 110 से अधिक ग्रामीण-सुरक्षाकर्मी खत्म होना छोटी बात नहीं है। हम अभी जिंदगी की कीमत की तुलना में सुरक्षा बलों पर हो रहे बहुत बड़े खर्च को भी नहीं गिन रहे हैं, लेकिन 60 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मी छत्तीसगढ़ के नक्सल मोर्चे पर तैनात हैं, और उन पर देश-प्रदेश का बहुत बड़ा खर्च तो हो ही रहा है। इसलिए नक्सलियों की शिकस्त के इस दौर में सरकार को सुरक्षा कार्रवाई जारी रखते हुए भी शांतिवार्ता की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि मौतें सिर्फ नक्सलियों की नहीं हो रही हैं।
ऐसा लगता है कि नक्सलि हिंसाग्रस्त इलाकों में सरकार की ढांचागत सुविधाओं, और जनकल्याण की योजनाओं के कुछ या अधिक हद तक कामयाब होने से भी जनता के बीच नक्सलियों का असर घटा होगा, और सुरक्षा बलों को पहले के मुकाबले कुछ अधिक जनसमर्थन मिल रहा होगा। इन बातों को अधिक बारीक हद तक आंकने का कोई जरिया हमारे पास नहीं है, लेकिन नक्सल इलाकों में चुनावों में जनता की भागीदारी और इन इलाकों में बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों के पीछे सरकारी योजनाओं की कामयाबी जरूर रही होगी। नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ा जा सकता, और आम जनता का लोकतंत्र पर भरोसा दुबारा कायम करना होगा, मजबूत करना होगा, और उसे जारी रखना होगा। यहां पर राजनीतिक और प्रशासनिक तबकों की जिम्मेदारी आती है।
किसी सुरक्षा विशेषज्ञ को इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि पांच बरस के कांग्रेस राज में यही सुरक्षा बल इसी नक्सल मोर्चे पर इतना शांत, चुप, या असफल क्यों था? और भाजपा सरकार आने से इसकी कामयाबी में इतना इजाफा क्यों और कैसे हुआ है? हम इस जटिल मुद्दे का अतिसरलीकरण करना नहीं चाहते हैं, किसी जानकार का एक अध्ययन और विश्लेषण के बाद ऐसा करना बेहतर होगा। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
केरल हाईकोर्ट ने अभी एक मामले में कहा ही था कि किसी व्यक्ति के शरीर को लेकर मोटा, पतला, ठिंगना, ऊंचा, सांवला, बहुत काला ऐसा कुछ भी कहने से परहेज करना चाहिए क्योंकि यह लोगों में शर्मिंदगी पैदा होने का काम होता है। जिस दिन हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की उसी दिन केरल के मलप्पुरम में एक 19 बरस की लडक़ी ने खुदकुशी कर ली जो कि अपने पति और उसके परिवार द्वारा रंग को लेकर लगातार की जा रही आलोचना से थक चुकी थी। इन दिनों अंग्रेजी बोलचाल में जिसे बॉडी-शेमिंग कहते हैं, बदन को लेकर शर्मिंदगी पैदा करने का यह काम हिन्दुस्तान में सबसे अधिक रंग को लेकर होता है। शादी के इश्तहार देखें तो हर किसी को गोरी लडक़ी चाहिए। जाति के साथ-साथ गोरे रंग की बराबरी की मांग रहती है। और गोरेपन से लेकर सांवलेपन के बीच कई शेड रहते हैं, जिन्हें लोग स्टूडियो की कलाकारी से बदलते हैं, या शब्दों में काले को सांवला, सांवले को गेहुंआ, गेहुंए को गोरा लिखने की भी कोशिश की जाती है। दुल्हन ढूंढते हुए तो काले लडक़ों के लिए भी मां-बाप गोरी दुल्हन तलाशते हैं ताकि अगली पीढ़ी का रंग कुछ ‘सुधर जाए’।
लेकिन रंगभेद महज हिन्दुस्तान में नहीं है, और कोई नई बात भी नहीं है। पूरी दुनिया में रंगभेद का भयानक इतिहास रहा है। इंसानों के बीच रंगभेद का नतीजा यह हुआ है कि लोग दुनिया भर के दूसरे कामों में भी रंगभेद करने लगे हैं, और लंबे समय से करते आए हैं। इस चर्चा को कहां से शुरू करें, और कहां खत्म करें, यह तय करना बड़ा मुश्किल है। अभी हिन्दुस्तान के दो-तीन बिल्कुल ही नौजवान खिलाडिय़ों ने शतरंज में बड़ी कामयाबी पाई है। अब शतरंज काली और सफेद गोटियों से खेला जाने वाला खेल है। यह पूरी तरह बिसात पर चली जाने वाली चालों का खेल है, लेकिन लोगों के दिमाग में काले और सफेद का फर्क ऐसा है कि काली गोटियों से खेलने वाले कुछ दबाव में रहते हैं, कि उनकी जीत की संभावना कम रहेगी। किसी जानकार ने 1851 से लेकर अब तक काली और सफेद गोटियों से खेलने वाले लोगों और उनमें से जीत पाने वाले लोगों का हिसाब लगाया है तो सफेद गोटियां काली के मुकाबले अधिक जीतती हैं। इसके साथ-साथ यह बात भी है कि खेल जैसे-जैसे ऊपर दिग्गज दर्जे पर पहुंचने लगता है, वैसे-वैसे सफेद की संभावना और बढ़ती जाती है। जिस किसी धारणा से भी सफेद गोटी वाले खिलाड़ी को अधिक आत्मविश्वास मिलता होगा, और काली गोटी वाले खिलाड़ी निराश होते होंगे, दिलचस्प बात यह है कि हिन्दुस्तान के दक्षिण भारत के सबसे सांवले या काले लोग भी शतरंज में सबसे कामयाब रहे हैं। इसी तरह एक दूसरे खेल को देखें जो कि हिन्दुस्तान में सडक़ किनारे भी खेला जाता है। कैरम की काली और सफेद गोटियों का मूल्य देखें तो काली गोटियों का मूल्य दस-दस रहता है, और सफेद गोटियों का बीस-बीस। अब रंगों को लेकर खिलाडिय़ों पर फर्क पड़ता है, या किसी रंग को नीचा दिखाने के लिए उसका दाम इस तरह रखा गया है, यह सोचने की बात है।
एक दूसरी मिसाल देखें जो कि रंगभेद की एक बड़ी ज्वलंत मिसाल है। दुनिया भर में सबसे मशहूर फैंटम और मैन्ड्रेक के कॉमिक्स देखें तो फैंटम एक गोरा व्यक्ति है जो कि अफ्रीका के जंगलों में बौने, काले लोगों को मुसीबतों से बचाने के लिए वहां जाता है, रहता है, और पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक ही नकाब में जीते हुए वह पूरी काली नस्ल की रक्षा करता है। उसे काले, बौने अफ्रीकी आदिवासी ईश्वर की तरह पूजते हैं, और जो पढऩे वाले लोगों के दिमाग में यह साफ-साफ तस्वीर बना देता है कि काले लोगों को बचने के लिए एक गोरे ईश्वर की जरूरत रहती है। दूसरी कॉमिक्स मैन्ड्रेक की देखें तो यह एक गोरा जादूगर है जो दुनिया के मुजरिमों और बुरे लोगों से भिड़ता है, और उसका सहयोगी लोथार नाम का एक अफ्रीकी राजकुमार है जो अपने राजपाठ को छोडक़र एक सेवक की तरह मैन्ड्रेक के साथ साये जैसा रहता है। अब एक अफ्रीकी राजकुमार को क्यों किसी अमरीकी गोरे जादूगर के अंगरक्षक-सहायक की तरह रहना चाहिए? लेकिन रंगभेद को बच्चों के मन में शुरू से ही गहरे जमा देने की यह एक गोरी चाल के अलावा और कुछ नहीं है। गोरी पश्चिमी दुनिया में ऐसी और भी बहुत सी मिसालें फिल्मों में देखने मिलती हैं। फिल्मों में यह बात कई बार मुद्दा रही कि कब कोई काला जेम्स बॉंड बनेगा? पश्चिमी दुनिया से निकली और दुनिया भर में सबसे मशहूर गुडिय़ा बार्बी 1959 में बाजार में उतारी गई, लेकिन पहली काली बार्बी 1980 में बाजार में आ पाई, और इसे लेकर इन 21 बरसों में खूब लिखा गया था।
हम हिन्दुस्तान में बच्चों के लिए लिखे गए एक गाने की चर्चा पहले भी कर चुके हैं, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा काले चोर ले गए। अब यह बात बच्चों के मन में इस बात को बिठा देती है कि चोर काले रंग के होते हैं। इसका दूसरा असर यह होता है कि उनमें से कुछ बच्चे चार कदम आगे बढक़र यह भी सोच सकते हैं कि काले लोग चोर होते हैं। गोरी अंग्रेज दुनिया में काले लोगों के खिलाफ कई किस्म की भाषा चलती है, और सभ्यता के विकास के साथ-साथ उनमें से कई शब्दों के खिलाफ कानून भी बना है। लेकिन काले रंग को नकारात्मक, और प्रतिरोध या विरोध का प्रतीक जाने-अनजाने बना दिया गया है। काले झंडे दिखाए जाते हैं, काली रिबिन बांधी जाती है, काला बाजारी होती है, ब्लैक मार्केटिंग, सिनेमा टिकट ब्लैक में बिकती है, सीमेंट ब्लैक मार्केट में बिकता है, हम बचपन से जितना पढ़ते आए हैं काले रंग को लेकर नकारात्मक के अलावा और कुछ नहीं दिखा है। लोग यह लिखते हैं कि फलां का नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इस तरह की मिसालें अंतहीन हैं। ईसाई दुनिया में मौत काले लबादे में आती है, और हिन्दुओं में यमराज काले भैंसे पर सवार होकर आता है। यमदूत कभी गोरे नहीं दिखाए जाते, और मौत को लेकर बनने वाले लतीफों को ब्लैक ह्यूमर कहा जाता है। इस तरह हमारी पूरी सांस्कृतिक सोच काले रंग को नकारात्मक बनाने की चली आ रही है। इसलिए कोई हैरानी नहीं है कि भारत जैसे देश में किसी सांवली या काली लडक़ी को ताने मार-मारकर खत्म कर दिया जाता है, उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया जाता है। रंगों की राजनीति को कुछ खुले दिल-दिमाग से समझने की जरूरत है, उसके बिना गांधी को उनके रंग के कारण गोरों के राज वाले अफ्रीका की ट्रेन से बाहर फेंक देना जारी रहेगा। ऐसी हो सोच के चलते केरल में इस नौजवान बहू को ससुराल में खुदकुशी करनी पड़ी। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
मध्यप्रदेश के एक जैन धर्मगुरू बताए गए मनोज भैय्याजी का एक वीडियो देखने मिल रहा है जिसमें वे प्रदेश में जैन मंदिरों पर हिन्दू संगठनों के हमलों पर नाराजगी और निराशा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो में बहुत कुछ कहा है, लेकिन हम हफ्ते-दस दिन पहले के ऐसे हमलों में जयश्रीराम के नारे लगाते हुए हिन्दू संगठनों को जैन मंदिरों पर हमला करने की खबरें भी देखते आए हैं, और उसके वीडियो भी देखकर हक्का-बक्का हैं। अभी कल तक की तो बात थी कि जैन समाज राम मंदिर से लेकर बाकी तमाम विवादास्पद हिन्दू मुद्दों पर हिन्दुओं के साथ खड़ा दिखता था। जबकि धर्मस्थलों के मालिकाना हक के बहुत से विवाद ऐसे रहते आए हैं जिनमें ऐसे कई मंदिर रहे हैं जो कि जैनों के थे लेकिन बाद में हिन्दुओं ने उन पर कब्जा करके उन्हें हिन्दू मंदिर बना लिया था। जैन उन पर वापिस कब्जा भी नहीं मांगते, और दूसरी जगहों पर हिन्दू कब्जे में वे हिन्दुओं का साथ देते हैं। ऐसे में इतनी जल्दी जैनों पर हिन्दू हमला हो जाए यह बड़ी अटपटी बात थी, लेकिन मध्यप्रदेश में पिछले ही पखवाड़े यह हुआ है। सागर में जयश्रीराम के नारों के साथ ऐसा हमला हुआ और उसकी पुलिस रिपोर्ट भी हुई है।
दरअसल न सिर्फ भारत का, बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास यह बताता है कि पहले तो किसी धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों से खूनी मुठभेड़ होती है, लेकिन जैसे-जैसे दूसरे धर्म के ‘दुश्मन’ घटते जाते हैं, वैसे-वैसे लोग फिर अपने धर्म के ही लोगों में दुश्मन ढूंढने लगते हैं। दुनिया में ईसाईयों के बीच कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदायों के बीच कितने खूनी संघर्ष नहीं हुए, उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट में सडक़ किनारे फुटपाथों पर ईसाई धर्म के इन दो समुदायों के निशान देखे जा सकते हैं, और एक-दूसरे के इलाके में घुसने का मतलब जान से हाथ धो बैठना भी होता है। (अब यह बात इस संपादक ने वहां 25 बरस पहले देखी थी, और हो सकता है कि अब तस्वीर कुछ बदली हो।) पाकिस्तान से आने वाली कितनी ही खबरें बताती हैं कि वहां मुस्लिमों के अलग-अलग कई सम्प्रदायों के बीच खूनी हमले होते हैं, और एक-दूसरे को थोक में मार डाला जाता है। वहां पर अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं माना जाता, और उन्हें निशाना बनाकर मारा जाता है, या कई मामलों में उनको पुलिस थाने से खींचकर बाहर निकालकर उनकी भीड़त्या की जाती है। भारत में भी इतिहास हिन्दुओं के भीतर संघर्ष और टकराव से भरा हुआ है। इंटरनेट पर मामूली सी सर्च बताती है कि वैदिक और तपस्वी परंपराओं के बीच टकराव होते रहा, शैव और वैष्णवों के बीच टकराव रहा, और हिन्दुओं का बौद्ध और जैन लोगों से टकराव का लंबा इतिहास है। हिन्दू धर्म से निकली हुई शाखाओं के साथ हिन्दू धर्म का टकराव सदियों तक चला।
मध्यप्रदेश में जिस तरह से सागर में हिन्दू और जैन टकराव खड़ा हुआ है, वह बहुत भयानक है। जैन अपने आपमें सीमित रहने वाला समुदाय है, न तो वह कोई धर्मांतरण करता, न ही किसी से नाहक टकराव करता, जैन धर्म में बाकी लोगों के शामिल होने की बात भी सुनाई नहीं पड़ती, इसलिए भी हिन्दुओं के साथ उनके टकराव की कोई आशंका नहीं बनती है। फिर भी चाहे स्थानीय मुद्दों को लेकर ऐसा बखेड़ा खड़ा हुआ हो, यह निराशा की बात तो है ही। फिर लोगों को यह भी समझने की जरूरत है कि आज देश में जिन दूसरे अल्पसंख्यक धर्मों के साथ हिन्दुत्व के लोगों का टकराव चल रहा है, उसमें एक मामूली समझदारी तो यह होनी ही चाहिए थी कि जैन जैसे लोगों को साथ रखा जाता।
दरअसल दिक्कत यह खड़ी हो जाती है कि जब अपनी जाति या धर्म के नाम पर टकराव का हिंसक मिजाज खड़ा होने लगता है, तो कुछ वक्त गुजर जाए, और हिंसा करने न मिले, तो हाथ खुजाने लगते हैं। जब धर्म के नाम पर टकराव और हिंसा की गुंजाइश कम हो जाती है, तो फिर लोग एक धर्म के भीतर सम्प्रदाय के टकराव खड़े करने लगते हैं, हिन्दुओं के भीतर जातियों के टकराव खड़े होने लगते हैं। हम पिछले कुछ अरसे में अपने आसपास लगातार हिन्दुओं के भीतर अलग-अलग जातियों के लोगों के बीच हिंसा के इक्का-दुक्का मामलों को जातियों के टकराव में बदलते भी देख रहे हैं। यह सिलसिला खतरनाक है जब लोग हर वक्त किसी दुश्मन के साथ ही जीने के आदी हो जाते हैं। जाहिर तौर पर कोई असली दुश्मन सामने न रहे, तो भी लोग हवा में दुश्मन ढूंढने लगते हैं, हवा में लाठियां चलाने लगते हैं। लोग इतनी मामूली समझ भी भूल जाते हैं कि कृष्ण के प्रेम से भरे इस देश में कालीदास के तमाम श्रंगार रस को अनदेखा करके लोग नौजवान प्रेमीजोड़ों पर हमला करने के लिए घर से लाठियों पर तेल लगाकर निकलते हैं। ऐसे जोड़ों का हिन्दू-गैर हिन्दू होना जरूरी नहीं रहता, हिन्दू धर्म के भीतर के लोगों को भी प्रेम करने पर मार डाला जा रहा है, और जब अपने ही धर्म के भीतर, अपनी ही जाति के भीतर हिंसा की गुंजाइश नहीं बचती, किसी दूसरी जाति से टकराव नहीं बचता, तो लोग परिवार के भीतर ही बेटियों को मर्जी का प्रेम करने पर ऑनरकिलिंग के नाम पर मार डालते हैं।
इस तमाम सच्चाई को देखकर एक ही बात समझ में आती है कि जब लोगों के मिजाज में ही भेदभाव, नफरत, और हिंसा को कूट-कूटकर भर दिया जाता है, तो उनके दिल-दिमाग से ये ही चीजें बाहर निकलती हैं। अगर देश-दुनिया को नफरत से बचाना है, तो छांट-छांटकर किसी धर्म, किसी जाति, किसी उपजाति के खिलाफ नफरत भरना, और बाकियों के प्रति प्रेम रखना कामयाब नहीं हो सकता। जब मिजाज ही नफरती हो जाता है, तो फिर वह नफरत अपनी जुगाली के लिए, अपना शौक पूरा करने के लिए कोई न कोई काल्पनिक दुश्मन गढ़ ही लेती है। जब धर्म और जातियां भी दुश्मन गढऩे के लिए काफी नहीं होते, तो फिर लोग पहरावे और खानपान को मुद्दा बनाकर नफरत और हिंसा की गुंजाइश निकाल लेते हैं। तीन चौथाई मांसाहारी आबादी वाले इस देश में बची एक चौथाई आबादी के एक बहुत से छोटे हिस्से की जिद से खानपान की हिंसा चल रही है।
लोगों को हिंसक और नफरती सोच के खतरों को इसलिए भी समझना चाहिए कि एक बार जब दिल-दिमाग में ये दो बातें बैठ जाती हैं, तो फिर वे अगली पीढिय़ों तक भी आगे बढ़ती हैं। हिंसा को खिला-पिलाकर पालना, और उसे नफरत की पीठ पर बैठाकर तबाही के लिए रवाना करना आत्मघाती ही होता है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
आंध्र के मुख्यमंत्री चन्द्राबाबू नायडू ने कुछ समय पहले कही अपनी बात फिर दोहराई है कि दो से कम बच्चों वाले मां-बाप को स्थानीय संस्थाओं के चुनाव लडऩे न मिले। वे पिछले कुछ समय से लगातार यह तर्क दे रहे हैं कि दक्षिण भारत के राज्य अपनी आबादी लगातार खो रहे हैं, और लोग बच्चे पैदा करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। आज भी आंध्र की आबादी बढऩा रूक गया है, और घटना शुरू हो गया है। भारत बहुत से अलग-अलग देशों का एक संघ सरीखा है जिसमें कुछ राज्यों की आबादी अभी भी बहुत बढ़ रही है, और कुछ राज्यों की बढऩा थम गई है। दिलचस्प बात यह है कि 1994 में अविभाजित आंध्र के मुख्यमंत्री की हैसियत से चन्द्राबाबू नायडू ने ही आबादी घटाने के लिए एक अलग नीति बनाई थी। अभी नायडू ने अपनी 1994 की एक नीति को बदला है जब वे आंध्र के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने पंचायत-म्युनिसिपल चुनावों में दो से अधिक बच्चों वालों के चुनाव लडऩे पर रोक लगा दी थी। 1990 का दशक कुछ उसी किस्म का था, और भारत सरकार की राष्ट्रीय विकास समिति की एक कमेटी ने उस वक्त यह सिफारिश की थी कि पंचायतों से लेकर केन्द्र सरकार की नौकरियों तक, तमाम सरकारी ओहदों पर दो या दो से कम बच्चों की सीमा लगानी चाहिए, और एक-एक करके देश के बहुत से राज्यों ने इसे लागू भी कर दिया था जिनमें मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल थे। बाद के बरसों में कुछ राज्यों ने इस शर्त को ढीला किया था, वरना इसके चलते पंच-सरपंच के निर्वाचित पद खत्म हुए जा रहे थे, अगर उन्हें तीसरा बच्चा होता था तो। इसे लेकर कई किस्म के पारिवारिक और सामाजिक तनाव भी हो रहे थे। अब चन्द्राबाबू नायडू ने 30 बरस बाद अपनी ही इस पुरानी नीति को खत्म किया है, तो इसके पीछे उनकी कही गई वजहों से परे भी कुछ दूसरी वजहें हो सकती हैं।
चन्द्राबाबू नायडू ने अभी कहा है कि आंध्र की आबादी बूढ़ी होती जा रही है, जवान कामकाजी लोग प्रदेश और देश छोडक़र बाहर चले जा रहे हैं। यह बात बहुत हद तक सही है, और आंध्र के साथ-साथ यह दक्षिण के अन्य राज्यों पर भी लागू होती है। आज दुनिया भर में हिन्दुस्तान से गए हुए जितने भी लोग जहां बसे हैं, उनमें दक्षिण भारतीय लोगों की बहुतायत है। इसके अलावा बहुत किस्म के तकनीकी कामों के लिए हिन्दुस्तान में देश भर में इंजीनियर और टेक्नीशियन दक्षिण भारत से आए हुए मिलते हैं। इस वजह से भी वहां की आबादी कम हो रही है, और अधिक शिक्षित और जागरूक लोग कम बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने में अधिक भरोसा रखते हैं। उत्तर भारत और हिन्दीभाषी राज्य इसके ठीक उल्टे चलते हैं, वहां पर कम लोगों को ही भविष्य और वर्तमान की अधिक फिक्र है, वहां से बहुत कम कामगार बाहर के पढ़े-लिखे और टेक्निकल कामों के लिए जाते हैं। उत्तर भारत से अधिक से अधिक मजदूर ही दूसरे प्रदेशों में जाते हैं जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था में कुछ अधिक जोडऩे की हालत में नहीं रहते। इसलिए अगर आंध्र में कामकाजी आबादी बाहर चली जा रही है, बुजुर्गों की देखभाल करने को लोग कम हैं, तो नायडू का तर्क सही है।
हमारा यह भी मानना है कि जो राज्य अपने नागरिकों पर सरकारी लागत से अधिक कमाई उन लोगों की दीगर कमाई से करता है, उसे अपनी आबादी बढ़ाने का एक नैतिक अधिकार रहता है। भारत में कुछ राज्य अपने लोगों को अनुदान देकर जिंदा रखते हैं, और कुछ दूसरे राज्य अपने लोगों की कमाई से स्थानीय अर्थव्यवस्था को विकसित होते देखते हैं, और उनसे टैक्स भी पाते हैं। इसलिए नायडू के प्रदेश में बढ़ती आबादी उन पर बोझ न होकर उनके लिए दुधारू गाय, या फलदार वृक्ष जैसी हो सकती है, जिसे बढ़ाने में उनकी दिलचस्पी हो। यह किसी सरकार की कामयाबी या नाकामी रहती है कि उसके लोग कितने उत्पादक बन पाते हैं। यह लोगों की अपनी खुद की परख का पैमाना नहीं रहता, यह सरकार की दूरदर्शिता, कल्पनाशीलता, और उसकी योजनाओं का सुबूत रहता है। दुनिया के कई देश आज सबसे अधिक विकसित होने के बाद भी आबादी लगातार खोते जा रहे हैं क्योंकि वहां लोग कमाने में ऐसे डूबे कि उन्होंने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी को बोझ की तरह पाया। ऐसे देशों की मिसाल देकर नायडू ने कहा है कि अगर प्रति जोड़े 2.1 से कम बच्चे होते हैं, तो वहां की आबादी गिरती चली जाना तय है। और दक्षिण कोरिया, जापान, इटली, जैसे बहुत से देश आज इस खतरे में घिर गए हैं।
आबादी के साथ एक बड़ी बात यह भी रहती है कि इसे लेकर जो नीतियां बनाई जाती हैं, उसका पहले तो समाज पर असर पडऩा शुरू होने में एक-दो पीढ़ी का वक्त लगता है, और फिर जब असर पडऩा शुरू होता है, तो लडख़ड़ाए कदमों को संभलने में फिर एक-दो पीढ़ी लग जाती है। इसलिए आबादी में फेरबदल बिजली की बटन दबाने की रफ्तार से नहीं हो पाता। किसी भी देश या प्रदेश को ऐसी नीतियां बनाने के पहले बहुत दूर की सोचनी चाहिए, वरना एक बच्चे की नीति पर चलते हुए चीन की आज लाख कोशिश के बावजूद लोग दो बच्चों पर भी नहीं आ पा रहे हैं, और अभी लगातार तीसरे साल उसकी आबादी में गिरावट दर्ज हुई है।
एक और बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि जब कभी आबादी को दो बच्चों तक सीमित रखा जाता है, तो आज भी गर्भ परीक्षण के कई गैरकानूनी तरीकों की वजह से पहले-दूसरे बच्चे के बेटे होने की संभावना अधिक रहती है, और पहले बच्चे के बेटी होने की नौबत कुछ कम आती है। इसकी वजह से भी समाज में लड़कियों का अनुपात गिर रहा था, अभी भी गिर रहा है। और कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि जब कभी जनसंख्या की नीतियां अधिक कड़ाई से लागू की जाती हैं, और दो बच्चों का नियम बनाया जाता है, तो लोग जांच की अपनी तरकीबें निकाल लेते हैं, और ऐसे बच्चों में लड़कियों का अनुपात कम रहता है। फिर भी हम आंध्र सीएम की बात को उसी राज्य के लिए ठीक मानते हैं क्योंकि वहां पर लोगों के पास रोजगार है, ऐसा हुनर पाने का जरिया है कि वे दुनिया भर में जाकर काम कर रहे हैं। आज अमरीका में कोई छोटा सा शहर भी ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई तेलुगु न बसे हुए हों। लेकिन बाकी देश जहां पर अधिकतर आबादी खेत और खदान मजदूर है, जहां पर सरकार का जनता पर खर्च अधिक होता है, और जनता से उतनी उत्पादकता नहीं मिलती है, उन प्रदेशों को आबादी बढ़ाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और कोई सोच भी नहीं रहे हैं।
अब आखिरी में एक मुद्दा रह जाता है जिसकी वजह से भी चन्द्राबाबू नायडू या दक्षिण के कुछ दूसरे नेता अधिक आबादी के हिमायती हैं। देश में जनगणना के बाद संसदीय और विधानसभा सीटों का डीलिमिटेशन होना है। विधानसभा सीटों से तो प्रदेश को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लोकसभा की सीटें आबादी के अनुपात में कम रह जाएंगी, तो दक्षिण भारत से सांसद घटेंगे, और देश की सरकार और संसद में दक्षिण की आवाज कमजोर होगी। इसलिए भी दक्षिण के नेता अब इस फिक्र में हैं कि देश की जनसंख्या नीति के मुताबिक आबादी को काबू में रखना उनके लिए आत्मघाती साबित हो रहा है, और संसद में उनकी गिनती घटने का खतरा आ खड़ा हुआ है। इसलिए नायडू की इस नई सोच के बहुत से अलग-अलग आयाम हैं, और देश के तमाम सोचने वाले लोगों को इन पहलुओं पर बात करनी चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखा है कि दिल्ली मेट्रो में छात्रों को रियायत दी जाए। उन्होंने लिखा कि स्कूल-कॉलेज जाने के लिए दिल्ली के छात्र बड़े पैमाने पर मेट्रो पर निर्भर रहते हैं। उन्हें 50 फीसदी की छूट दी जानी चाहिए ताकि उन पर बोझ कम हो। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली मेट्रो दिल्ली सरकार, और केन्द्र सरकार के आधे-आधे लागत वाली परियोजना है, इसलिए छात्रों को इस प्रस्तावित रियायत को राज्य और केन्द्र सरकार आधा-आधा दें। उन्होंने यह भी लिखा है कि वे छात्रों के लिए बस यात्रा पूरी तरह मुफ्त करने की योजना बना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में 20 दिनों के भीतर ही, 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव हैं, और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। ऐसे में दस बरस से अधिक से दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी का मतदान के ठीक पहले का यह प्रस्ताव नौजवान वोटरों, और उनके परिवारों के लिए चुनावी रेवड़ी सरीखा भी लग सकता है। लेकिन इस शहर से परे, और इस चुनाव से परे भी इस सोच पर चर्चा होनी चाहिए।
हिन्दुस्तान में दर्जनों ऐसे शहर हैं जिनका विस्तार दस-बीस किलोमीटर से अधिक हो चुका है, और वहां पर लोगों की आवाजाही में बसों का बड़ा इस्तेमाल है। करीब डेढ़ दर्जन शहरों में मेट्रो भी चल रही हैं, और उन शहरों को इसका बड़ा सहारा है। मेट्रो और बस के बिना इन शहरों में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की आवाजाही की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन शहरी योजना में बड़ी खामियां और कमजोरियां हैं, कल्पनाशीलता की कमी है, और आज भी अधिकतर शहरों में आबादी का एक बड़ा हिस्सा निजी गाडिय़ों पर निर्भर करता है क्योंकि सार्वजनिक परिवहन उन्हें सिरे से सिरे तक नहीं पहुंचा पाता। दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली का ही हाल यह है कि साल में कुछ महीने वहां कई तरह के प्रदूषण जीना हराम कर देते हैं, और ऐसे में निजी गाडिय़ों से होने वाला प्रदूषण भी बहुत रहता है। इसलिए दुनिया के दूसरे विकसित देशों की तर्ज पर हिन्दुस्तान के शहरों में भी सार्वजनिक परिवहन को लगातार बढ़ाना जरूरी है, और इसे तेज रफ्तार से बढ़ाना इसलिए चाहिए कि लोग निजी गाडिय़ां खरीद लें, उसके पहले उन्हें अगर सहूलियत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाए, तो वे खरीदने से रूक सकते हैं।
दुनिया के विकसित देशों से भारत की आबादी की तुलना बहुत आसान नहीं है, और न ही वहां की सरकारों की क्षमता से भारत के देश-प्रदेश की सरकारों की आर्थिक ताकत की तुलना की जा सकती। लेकिन प्रदूषण का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है, और इसमें वाहनों का प्रदूषण एक बड़ा हिस्सेदार है जो कि कम किया जा सकता है। इसे बिजली और बैटरी से चलने वाली गाडिय़ों के रास्ते भी घटाया जा सकता है, सार्वजनिक परिवहन बढ़ाकर और निजी गाडिय़ों को कम करके भी किया जा सकता है। ऐसे में केजरीवाल का अभी सामने रखा गया प्रस्ताव चाहे एक चुनावी शिगूफा हो, इसे एक मुद्दा मानकर चुनाव के बाद भी देश भर में इस पर चर्चा हो सकती है। बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण पूरी दुनिया बहुत किस्म के नुकसान झेल रही है। आज की ही एक रिपोर्ट बताती है कि मौसम की मार से हिन्दुस्तान में फसल का कितना नुकसान हुआ है। मोंगाबे-इंडिया की 2022 की एक रिपोर्ट बताती है कि उसके पहले के छह बरसों में मौसम की सबसे बुरी बढ़ चली मार की वजह से करीब 7 करोड़ हेक्टेयर की फसल बर्बाद हुई। अब लोग सडक़ों पर गाडिय़ों के प्रदूषण से गिरती हुई उपज का रिश्ता सीधा नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन जब जलवायु परिवर्तन की बड़ी वजहों को देखेंगे, तो यह साफ-साफ समझ आएगा कि दुनिया को सार्वजनिक परिवहन की तरफ की कितनी जरूरत है। इसके साथ-साथ इस बात को भी समझना होगा कि सडक़ों के प्रदूषण से शहरी इंसानों की सेहत किस हद तक खराब हो रही है, वे किस हद तक सांस की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, और उनमें कैंसर का खतरा कितना बढ़ रहा है। इन सबको भी राष्ट्रीय उत्पादकता के साथ जोडक़र देखने की जरूरत है, और वह बहुत आसान नहीं है। इसलिए धरती और इंसान दोनों की सेहत गाडिय़ों की बढ़ती संख्या और उनके प्रदूषण से बर्बाद हो रही है, और इससे बचाने का फिलहाल तो अकेला जरिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट है।
योरप के कुछ संपन्न देशों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सौ फीसदी मुफ्त कर दिया है। कुछ और जगहों पर इसके साथ-साथ लोगों को जागरूक बनाने के लिए कई मौलिक प्रयोग किए जा रहे हैं। मेट्रो या बस की टिकट मशीन के सामने उठक-बैठक जैसी कसरत करने पर भी टिकट मुफ्त मिल जाती है, या ुकुछ जगहों पर खड़ी हुई साइकिल चलाकर उससे बिजली पैदा करने के एवज में ऐसी टिकट दी जाती है। समझदार देशों में लोग खुद होकर भी निजी गाडिय़ों का इस्तेमाल कम करते हैं, हालांकि अमरीका जैसे बेदिमाग और बददिमाग देश में लोग दानवाकार बड़ी-बड़ी गाडिय़ां रात-दिन दौड़ाते हैं। भारत को चूंकि अपनी आबादी को राशन और बिजली की रियायत सरीखी कई चीजें देनी ही रहती हैं, अलग-अलग पार्टियां, और अलग-अलग राज्य जनता को कई तरह की छूट दे रहे हैं, ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बड़ी रियायत, या पूरी छूट से शहर, शहरी, फेंफड़े, और पर्यावरण सब कुछ बच सकते हैं। आज निजी गाडिय़ों की बढ़ती भीड़ की वजह से जो महंगे फ्लाईओवर बनाने पड़ते हैं, रिंग रोड बनानी पड़ती हैं, उन सबकी लागत भी तो आती ही है। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढऩे से शहरी सडक़ों पर भीड़ भी घटेगी, और वैकल्पिक सडक़ें बनाने का अंतहीन सिलसिला भी थमेगा। चाहे आज की यह सलाह केजरीवाल की तरफ से आई हो, लेकिन इस पर दिल्ली का चुनाव निपट जाने के बाद पूरे देश में एक चर्चा होनी चाहिए, और सरकारों को दस-बीस बरस बाद के जलवायु परिवर्तन के खतरों को समझते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और उसकी रियायतों में पूंजीनिवेश करना चाहिए।
छत्तीसगढ़ के एक लोकप्रिय आदिवासी नेता, और बस्तर से छह बार के विधायक रहे कवासी लखमा को कल ईडी ने भूपेश सरकार के वक्त के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है। इस चर्चित शराब घोटाले में दो हजार करोड़ से अधिक के काले कारोबार का आरोप ईडी ने अदालत में लगाया है, और इस मामले में प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक दिग्गज अफसर और कारोबारी पहले से गिरफ्तार हैं। कवासी लखमा भूपेश सरकार में आबकारी मंत्री थे, और आबकारी विभाग की फाइलों पर वे बिना पढ़े दस्तखत करते थे क्योंकि वे पढऩा नहीं जानते, जाहिर तौर पर लिखना भी नहीं जानते, और सिर्फ दस्तखत करना जानते हैं। ऐसे कवासी लखमा को कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या सोचकर, या बहुत सोचकर आबकारी मंत्री बनाया था, और एक अनपढ़ आदिवासी उस कार्यकाल के लिए अब ईडी हिरासत में है, और गिरफ्तारी के बाद जेल पहुंचना महज वक्त की बात है। ईडी ने अदालत को बताया है कि पहले जिन बड़े अफसरों को गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने कवासी लखमा को हर महीने दो करोड़ रूपए देने का बयान दिया है, और लखमा ने इसी रकम में से परिवार का एक बड़ा सा घर बनवाया है, और सुकमा में कांग्रेस भवन भी। कांग्रेस भवन का हिसाब कांग्रेस पार्टी जाने, लेकिन कभी चुनाव न हारने वाला यह आदिवासी विधायक ईडी के जाल में फंस चुका है, और इसे लेकर लोगों के मन में रंज भी है।
दरअसल छत्तीसगढ़ को बेहतर तरीके से जानने वाले लोगों के बीच दो हजार करोड़ के शराब घोटाले की चार्जशीट पर किसी को हैरानी नहीं है। प्रदेश में शराब के धंधे और तौर-तरीके को लाखों लोग जानते थे, उन्हें यह हैरानी जरूर हो सकती है कि ईडी कुल दो हजार करोड़ के घोटाले का केस बना पाई है। जिन लोगों की गिरफ्तारी अब तक शराब घोटाले में हुई है, उनमें से किसी की भी मासूमियत का कोई धोखा किसी को नहीं है, और सबको यह पता है कि ये लोग पांच बरस किस तरह से आबकारी विभाग चला रहे थे। लोगों को यह भी उतनी ही अच्छी तरह मालूम था कि कवासी लखमा लिखना-पढऩा नहीं जानते, वे सिर्फ दस्तखत कर सकते हैं। ऐसे में आबकारी जैसा विभाग उन्हें देना, और फिर इतना बड़ा शराब घोटाला होना, इनमें कुछ भी मासूम नहीं था। अगर दो करोड़ रूपए महीने आबकारी मंत्री को दिए भी गए थे, तो हर महीने सैकड़ों करोड़ रूपए का घोटाला उनके मातहत विभाग में उनके दस्तखत से, या बिना दस्तखत के किया जा रहा था, और मंत्री को एक टुकड़ा डाल दिया जाता था। यह शायद हिन्दुस्तान के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी सदन में मंत्री ने अपने विभाग से जुड़े किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक सबसे भरोसे के, और ताकतवर मंत्री मो.अकबर ही पूरे पांच साल कवासी लखमा की जगह जवाब देते रहे। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए यह बात एक फिक्र की होनी चाहिए थी कि आबकारी जैसे बदनाम और विवादास्पद विभाग का मंत्री एक ऐसे सीधे-सादे, और अनपढ़ विधायक को बना दिया गया था जो कि खबरों में चारों तरफ बरसों से छाए रहने वाले इस विभाग पर कोई भी काबू नहीं पा सकता था। बरसों से देश का मीडिया और ईडी की अदालत आबकारी घोटाले की खबरों से भरे पड़े थे, और कांग्रेस पार्टी, छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल, विधानसभा, राज्यपाल, ये सारे के सारे मानो अनपढ़ बने हुए थे, इस विभाग का हर दारू दुकान पर दिखता घोटाला किसी को नहीं दिख रहा था। लोकतंत्र में यह देखना भी हैरानी की बात थी कि कांग्रेस मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने यह सवाल नहीं उठाया कि पढ़ न पाने वाले मंत्री से फाइलों पर दस्तखत कैसे कराए जा रहे हैं? शपथ दिलाने वाले राज्यपाल ने यह नहीं पूछा कि कवासी लखमा मंत्री की जिम्मेदारी कैसे पूरी करेंगे, और अपने आपको देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली कांग्रेस ने भी कभी आंख खोलकर यह नहीं देखा कि छत्तीसगढ़ से जिस आबकारी घोटाले की खबरें चारों तरफ उठ रही हैं, उस विभाग को कैसा मंत्री चला रहा है। कवासी लखमा खुद तो एक सीधे-सरल आदिवासी हैं, लेकिन उनके कंधे पर बंदूक रखकर जिन सारे लोगों ने यह शराब घोटाला किया है, उन नेताओं, और पार्टी को तो इसका जवाब देना होगा कि एक आदिवासी को इतना बदनाम करके जेल भिजवाने की सजा उनके कौन-कौन लोग पाएंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक अनपढ़ नेता को इस तरह फंसा देने की सजा अदालत चाहे न दे सके, कांग्रेस पार्टी को तो देना ही चाहिए। और शायद इस पूरे दौर में राहुल गांधी ही कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्हें कुछ देर आईने के सामने खड़े होकर कवासी लखमा की गिरफ्तारी के पीछे अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए। राहुल का ब्रिटेन की नामी यूनिवर्सिटी में पढऩा भला किस काम का अगर वे एक आदिवासी को फंसाने और जेल भिजवाने की साजिश के सक्रिय हिस्सेदार, या मूकदर्शक थे? लोगों को यह भी याद रखने की जरूरत है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए दो बरस से फरार हैं, उन्हें धरती निगल गई, या आसमान खा गया, अभी कुछ भी साफ नहीं है। परिवार वाला एक अरबपति कारोबारी बरसों से फरार है, और पार्टी के पास अपने इस कोषाध्यक्ष पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है, लोकतंत्र में ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने इतने बड़े, इतने प्रभावशाली, और इतने संपन्न पदाधिकारी की फरारी पर पार्टी कुछ भी न कहे।
हमारी बातें कांग्रेस और पिछली सरकार के मुखिया भूपेश बघेल को कुछ तल्ख और असुविधाजनक लग सकती हैं, लेकिन कवासी लखमा तो इस हालत में भी नहीं हैं कि उनके साथ हुई साजिश और बेइंसाफी के खिलाफ एक मजबूत बयान लिख सकें या दे सकें, ऐसे में किसी न किसी को तो कवासी लखमा का यह मुद्दा उठाना ही है कि बड़े-बड़े नामी-गिरामी नेताओं, अफसरों, और उनकी गिरोहबंदी वाले कारोबारियों ने मिलकर खुद तो हजारों करोड़ कमाए ही, एक अनपढ़ आदिवासी को बुरी तरह फंसा दिया। कांग्रेस नेताओं का यह तर्क किसी काम का नहीं है कि ईडी ने यह गिरफ्तारी पंचायत और म्युनिसिपल चुनावों को प्रभावित करने के लिए की है, यह कार्रवाई तो किसी भी तरह के चुनाव के बरसों पहले से चल रही है, और राज्य के एक पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड सहित कितने ही नेताओं, अफसरों, और कारोबारियों के यहां विधानसभा चुनाव के बरसों पहले से छापे पड़ते आए हैं। लोकतंत्र में चुनाव तो चलते ही रहते हैं, और सरकारी एजेंसियों की कार्रवाईयां भी चलती रहती हैं। खुद भूपेश सरकार की अधिकतर जांच एजेंसियों के नामी-गिरामी केस सुप्रीम कोर्ट तक जाकर बदनीयत के पाए गए, और खारिज हुए हैं। इसलिए हर बात को चुनाव से जोडक़र देखना ठीक नहीं है।
छत्तीसगढ़ बुनियादी तौर पर एक आदिवासी राज्य है, और एक सबसे कामयाब, सबसे लोकप्रिय निर्वाचित जनप्रतिनिधि को इस तरह घेरकर फंसाना आसानी से नहीं लिया जाना चाहिए। इसके लिए कवासी लखमा की अपनी पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं। लखमा खुद अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ सब कुछ जानते-समझते हुए भी कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन आदिवासी समाज को इस बारे में कांग्रेस से जवाब लेना चाहिए, और कटघरे में खड़ा करना चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
अमरीका भी गजब का देश है। कई मायनों में ऐसा लगता है कि वहां कारोबार और सरकार के बीच रिश्ते इतने लोकतांत्रिक रहते हैं कि किसी कारोबारी के किसी पार्टी के विरोधी रहने पर भी उस पार्टी की सरकार बनने पर उसके कारोबार पर कोई खतरा नहीं रहता। वहां की लोकतांत्रिक संस्थाएं कभी बड़ी मजबूत लगती हैं, तो कभी हैरान कर देने की हद तक अजीब लगती हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने अभी काम संभाला भी नहीं है कि उनके मनोनीत लोग छुट्टे सांडों की तरह चारों तरफ सींग मार रहे हैं। कुछ तो ऐसे लोगों को उन्होंने मनोनीत कर दिया जिनके बीते बरसों की कब्र फाडक़र कुछ विवादास्पद कंकाल निकले, और उन्हें खुद होकर इस मनोनयन से बाहर हो जाना पड़ा। दूसरी तरफ एलन मस्क जैसा दुनिया का सबसे रईस आदमी, और ट्रम्प के ही टक्कर का सनकी, बददिमाग, और शायद बेदिमाग भी, ऐसा साबित हो रहा है जैसा कि दुनिया में किसी ने कहीं देखा न होगा। एक तरफ तो वह सरकार के खर्च में कटौती के लिए ट्रम्प की तरफ से मनोनीत किया गया है, और दूसरी तरफ वह अमरीकी सरकार के साथ कारोबार करने वाला एक सबसे बड़ा अंतरिक्ष-कारोबारी भी है, वह कल के ट्विटर और आज के एक्स सरीखे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मालिक भी है, और वह ट्रम्प के शपथ ग्रहण के पहले ही दूसरे देशों की घरेलू नीतियों में जिस तरह सिर घुसा रहा है, उससे यह हैरानी होती है कि क्या किसी विकसित लोकतंत्र का राष्ट्रपति ऐसे पालतू सांड रख सकता है जो कि उसी की अपनी चीनी मिट्टी बर्तनों की दुकान को तहस-नहस करते रहें? अमरीकी सरकार में ट्रम्प पर सबसे अधिक असर जिस मस्क का रहेगा, जो कि राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के समय से ही ट्रम्प के घर में ही बसा हुआ है, वहीं से अपना कारोबार भी चला रहा है, और वहीं से सार्वजनिक रूप से दूसरे देशों के मामलों में भयानक दर्जे की दखल भी दे रहा है, वह शपथ ग्रहण के बाद जाने क्या करेगा? ट्रम्प का अपना मिजाज मैड मैन पॉलिसी वाला माना जाता है, यानी किसी पागल इंसान की नीतियों वाला। खासकर विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर ट्रम्प लोकतंत्र के पहले के दिनों में जाता हुआ दिख रहा है, और मानो उसकी अपनी बददिमागी काफी न हो, उसे एलन मस्क जैसा एक और सनकी तानाशाह सलाहकार भी मिल गया है।
पता नहीं अमरीका का लोकतंत्र किस किस्म का है कि एक सबसे अधिक पढ़े-लिखे, विकसित, कामयाब और कारोबारी देश के लोगों ने जिस अप्रत्याशित बहुमत से ट्रम्प जैसे घटिया, खतरनाक, तानाशाह, और सनकी को चुना है, वे अमरीका का किस तरह का भविष्य चाहते हैं, और बाकी दुनिया में अमरीका की भूमिका किस तरह की चाहते हैं। हम एक बार फिर एलन मस्क की बात पर लौटें, तो निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा मस्क और एक भारतवंशी अमरीकी कारोबारी विवेक रामास्वामी का सरकारी खर्च में कटौती के लिए मनोनयन किए जाने के बाद से मस्क ने अमरीका के भीतर के बारे में भी जितने किस्म के बयान दिए, उनसे ट्रम्प की अपनी रिपब्लिकन पार्टी भी बड़ी नाखुश हुई, लेकिन वहां कामयाब नेता पर शायद पार्टी का बहुत कम बस चलता है। अभी मस्क ने जर्मनी में एक धुर दक्षिणपंथी पार्टी को सार्वजनिक रूप से बढ़ावा दिया है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की इस बात के लिए आलोचना की है कि उन्होंने बरसों पहले ब्रिटेन में सामने आए एक सेक्स स्कैंडल की जांच में पर्याप्त दिलचस्पी नहीं ली थी जिसमें मोटेतौर पर पाकिस्तानी मूल के कई लोगों ने ब्रिटेन की नाबालिग गोरी लड़कियों को फंसाकर साजिश के तहत उनका यौन शोषण किया था। जर्मनी और ब्रिटेन के ये दोनों मामले किसी भी तरह अमरीका से जुड़े हुए नहीं हैं, और दोनों ही घरेलू मामलों में अमरीका की अगले हफ्ते बनने जा रही सरकार के एक सबसे असरदार कारोबारी को कुछ बोलने की जरूरत थी। लेकिन मस्क ब्रिटेन की घरेलू राजनीति में किसी पार्टी का साथ दे रहा है, तो जर्मनी में किसी दूसरी पार्टी का। खुले रूप में जब एलन मस्क ऐसा कर रहा है, तो सवाल यह उठता है कि अमरीकी राष्ट्रपति पर सबसे अधिक असर रखने वाला यह कारोबारी विदेश नीति को अघोषित रूप से किस तरह प्रभावित करेगा? एक सवाल यह भी उठ रहा है कि ट्रम्प ने एलन मस्क को अपना दायां हाथ बनाकर हितों के टकराव की एक नौबत भी खड़ी कर दी है क्योंकि मस्क की बैटरी कार की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, टेस्ला का बड़ा कारोबार दुनिया के कई देशों के साथ है, सेटेलाइट इंटरनेट का उसका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है, ऐसे में मस्क अमरीकी राष्ट्रपति के साथ रोज बैठते-खाते-पीते हुए उन देशों के साथ अमरीका की नीतियों को किस तरह प्रभावित करेगा? यह तो ठीक है कि अमरीकी राजनीति पर कारोबारियों का असर और उनकी पकड़ कोई बहुत नई बात नहीं है, लेकिन यह असर चुनाव चंदे के मार्फत आता था, और पर्दे के पीछे से काम करता था। एलन मस्क की शक्ल में यह राष्ट्रपति के सिर पर बैठकर काम कर रहा है, और ट्रम्प का मस्क पर जो अंधविश्वास दिख रहा है, वह अमरीका की घरेलू सरकारी नीतियों, और देश की विदेश नीति, इन दोनों पर बहुत बड़ा असर डालता दिख रहा है।
पता नहीं कोई लोकतंत्र दुनिया के सबसे रईस आदमी, और अमरीका के सबसे बड़े कारोबारी, और दर्जनों देशों तक फैले कारोबार वाले इस सनकी के दबाव और असर तले किस तरह काम कर सकता है? यह सरकार और कारोबार के संबंधों का एक बड़ा दिलचस्प मामला तो है, और इन विषयों के शोधकर्ताओं के लिए यह एक अच्छा सामान भी रहेगा। भारत जैसे लोकतंत्र में सरकार में कारोबारी दखल पर्दे के कुछ पीछे से चलती है, यहां पर कारोबारी खुद ही सरकार चला रहा है, खुद ही सरकार के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रहा है, और दुनिया के दूसरे देशों में सरकारों और राजनीतिक दलों को आगे-पीछे करने की अपनी सनक लाद रहा है। यह देखना हैरान करता है कि एक कारोबारी जिस तरह कार और अंतरिक्ष के अपने कारोबार से परे जाकर रातोंरात ट्विटर खरीदता है, और उसे अपनी सनक से बदलता है, वैसा कारोबारी अब दुनिया को बदलने की अपनी सनक अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय के मार्फत किस तरह लादेगा!
पश्चिम बंगाल की एक रिपोर्ट एक प्रमुख समाचार प्लेटफॉर्म, डाइचे वैले पर आई है जिसमें बताया गया है कि वहां तीन हजार से ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल चल रहे हैं जिनमें 23-24 शैक्षणिक सत्र में एक भी छात्र-छात्रा की भर्ती नहीं हुई। और इन स्कूलों में 14 हजार से अधिक शिक्षक हैं जो बिना काम तनख्वाह पाते रहे, और प्रदेश में 6 हजार से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ एक-एक शिक्षक हैं। देश में और राज्यों में भी आगे-पीछे इसी तरह की हालत है, बस यही कि पढ़ाई-लिखाई के लिए जाने जाने वाले बंगाल की यह बदहाली हो गई है। लोगों को याद होगा कि इस राज्य में शिक्षक भर्ती घोटाला में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की दखल से एक मंत्री सहित बहुत से दूसरे लोग गिरफ्तार हैं, और कोई हैरानी नहीं है कि स्कूलों की दर्ज संख्या गिरती जा रही है। वैसे स्कूलों में दर्ज संख्या के मामले में देश के बाकी राज्य भी बदहाली झेल रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। देश का कानून बाल मजदूरी के खिलाफ है, इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि बच्चे पढ़ाई छोडक़र मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन वे पढ़ाई की तरफ अधिक नहीं आ रहे हैं, यह तो एक सच्चाई है ही। दूसरी तरफ अनौपचारिक तौर पर यह पता लगता है कि बच्चे स्कूल आना बंद कर देते हैं तो भी जवाब-तलब से बचने के लिए स्कूल के शिक्षक और हेडमास्टर उनके नाम रजिस्टर से नहीं हटाते ताकि सरकार से कोई नोटिस न झेलना पड़े, और उन छात्रों के नाम से दोपहर के भोजन का खर्च, यूनिफॉर्म, और किताबें सब मिलते रहते हैं जो कि स्कूल के प्रभारी लोगों की ऊपरी कमाई हो जाती है। ऐसे में सरकार के दर्ज संख्या के आंकड़े बहुत विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर बताने में सबकी चमड़ी बची रहती है, और दमड़ी (पैसे) भी मिलते रहती है।
हिन्दुस्तान की हालत देखें तो आज ही सोशल मीडिया पर एक गंभीर व्यक्ति ने यह लिखा है कि हिन्दुस्तानी कामगार काम नहीं करते, नौकरी करते हैं। अब यह सोच निजी कंपनियों और संस्थाओं के कर्मचारियों के बारे में शायद सच न हो, क्योंकि वहां अधिक जवाबदेही रहती है, लेकिन सरकारी नौकरियों के बारे में तो यह सच है ही क्योंकि वहां नौकरी पाने के बाद रिटायर होने तक की एक ऐसी हिफाजत हासिल हो जाती है कि काम करें या न करें, तनख्वाह तो मिलते ही रहेगी। हम छत्तीसगढ़ में ही स्कूलों का हाल देखते हैं तो जगह-जगह मास्टर शराब पीकर पहुंचते हैं, स्कूल पहुंचकर शराब पीते हैं, स्कूल में फर्श पर पड़े रहते हैं, कुछ जगहों के वीडियो सामने आए जिनमें क्लास के बच्चों और प्रधानपाठिका के सामने बैठकर एक मास्टर दारू पीते रहा, हर दिन नशे में पहुंचने वाले एक मास्टर को स्कूल के छोटे बच्चे चप्पल मार-मारकर भगा रहे हैं, एक जगह मास्टर बंदूक लेकर प्रधानपाठिका को धमकाने पहुंच गया, एक जगह मास्टर शिक्षा विभाग की महिला अधिकारी का गला घोंटने लग गया, कोई हफ्ता ऐसी खबरों के बिना नहीं निकलता। जिन लोगों का बदअमनी का यह हाल है, वे वीडियो और खबरों से परे भी क्या पढ़ा लेते होंगे? छत्तीसगढ़ में भी राज्य छोटा होने के बावजूद सैकड़ों स्कूलें ऐसी है जहां एक-एक शिक्षक पांच-पांच क्लास पढ़ा रहे हैं, और शिक्षक संघों के दबाव में लोगों के तबादले नहीं हो पा रहे हैं।
जब देश में बुनियादी प्राथमिक शिक्षा का यह हाल है, तो इस बुनियाद पर खड़ी इमारत कैसी होगी? यहीं पर आकर दक्षिण भारत के राज्य उत्तर भारत को मीलों पीछे छोड़ देते हैं, और बाकी हिन्दी प्रदेशों को भी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़ाई की उत्कृष्टता पर दक्षिण में जो जोर दिया जाता है, उसी का नतीजा है कि बाकी दुनिया में सबसे अधिक हिन्दुस्तानी दक्षिण भारतीय राज्यों से ही जाते हैं। हिन्दी के तो अधिकतर राज्यों के अधिकतर लोग अपने ही राज्यों में बेरोजगार होने का गौरव हासिल करते हैं क्योंकि न तो सरकार उन्हें तैयार करती, और न ही सामाजिक रूप से उनके सामने अपने सीनियर छात्र-छात्राओं की कोई अच्छी प्रेरणा देने वाली मिसाल ही रहती। जिन राज्यों में पीढिय़ों से लोगों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए तैयार किया जा रहा है, वहां छात्रों की हर बैच के सामने दूसरे होनहार और कामयाब छात्र-छात्राओं की एक मिसाल रहती है, और यह मिसाल चुनौती की तरह भी रहती है। हिन्दी हिन्दुस्तान में ऐसी किसी चुनौती का दबाव नहीं रहता, और हर पीढ़ी के पास अपने से पहले की पीढ़ी के निठल्ले और बेरोजगार होने की बड़ी सहूलियत की मिसाल रहती है। हिन्दी के राज्यों से देश-विदेश में जाकर कामयाबी पाने की गिनी-चुनी कहानियां तो कोई सुना सकते हैं, लेकिन कोई संख्या नहीं बताई जा सकती, ये कहानियां उंगलियों पर गिनने जितनी ही रहती हैं।
पूरी विकसित दुनिया के सभ्य लोकतंत्र जिन दो चीजों पर सबसे अधिक गंभीरता से ध्यान देते हैं, वे प्राथमिक शिक्षा, और स्वास्थ्य हैं। भारत के जिन राज्यों में प्राथमिक शिक्षा की बुनियाद मजबूत रहती है, वहां पर लोग बड़े होने पर भी अधिक कामयाब होते हैं। लेकिन केन्द्र सरकार के किए हुए कई सर्वे बताते हैं कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मिडिल स्कूल में पहुंच चुके छात्र-छात्राओं को भी अपने से तीन-चार साल छोटी क्लास का जोड़-घटाना भी नहीं आता। स्कूलों से जो बच्चे कॉलेजों में पहुंचते हैं, वे कॉलेज की पढ़ाई शुरू करने लायक नहीं रहते। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को छत्तिसगढिय़ा सबले बढिय़ा जैसे आत्ममुग्ध नारों से मुक्ति पानी चाहिए, और हकीकत की कड़ी जमीन पर नंगे पैर खड़े होकर अपने आपको तौलना चाहिए कि राष्ट्रीय पैमानों पर दूसरे राज्यों के मुकाबले उसकी स्थिति क्या है। खदान की कमाई से खेतों को अनुदान देते चलने से हर बरस का काम तो चल रहा है, लेकिन अगर नौजवान पीढ़ी को देश के दर्जन भर विकसित राज्यों के बच्चों के मुकाबले तैयार नहीं किया जाएगा, तो दस-बीस बरस में इस राज्य की नई पीढ़ी हर किस्म के राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से बाहर रहेगी। जब कभी किसी दूसरे राज्य की खामियां सामने आती हैं, तो बाकी राज्यों को भी अपने आपको तौल लेना चाहिए, ऐसी समझदारी दिखाए बिना खुद ठोकर खाकर संभलने तक तो बड़ी देर हो चुकी रहती है, और बड़ा नुकसान हो चुका रहता है। छत्तीसगढ़ सरीखे हर राज्य को नारों से परे अपने आपको सचमुच ही बेहतर बनाने की जरूरत है, वरना हर बरस ये राज्य दक्षिण से कुछ और मील पीछे जाते रहेंगे। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
हर कुछ दिनों में आसपास से ऐसी खबर आती है कि नवजात शिशु को नाले या घूरे पर फेंका गया। कभी-कभी ये जिंदा भी रहते हैं, और अस्पताल इन्हें बचाने की भरसक कोशिश भी करते हैं, कभी वे बचा पाते हैं, कभी नहीं बचा पाते। उन नवजात शिशुओं की तकलीफ को बखान करने वाले लोग नहीं रहते, लेकिन बहुत आसानी से इस बात का अहसास किया जा सकता है कि जिन बच्चों को पैदा होने के बाद गोद से ही नहीं हटाया जाता, जिन्हें लिटाने के लिए पुराने घिसे हुए कपड़ों की गुदड़ी बनाई जाती है कि उनकी नाजुक चमड़ी को नुकसान न पहुंचे, ऐसे बच्चों को जब नालियों और घूरों में फेंक दिया जाता है, तो उनके साथ क्या गुजरती होगी? कभी-कभी ऐसे बच्चे नजर आने के पहले ही कुत्तों के शिकार हो जाते हैं, और या तो इनके कुछ अंग चले जाते हैं, या पूरी जान ही चली जाती है। फिर इसे समाज की इस हकीकत से जोडक़र देखने की जरूरत है कि किस तरह कुछ लोग बच्चों की चाह में दशकों तक पूजा-पाठ करते रहते हैं, चिकित्सा विज्ञान की सुविधाओं से कोशिश करते हैं, और फिर भी उन्हें बच्चे नहीं हो पाते। एक तरफ बच्चों की चाह में बहुत से जोड़े लगातार अंधाधुंध मेहनत और खर्च करते हैं, दूसरी तरफ कुछ अवांछित माने जाने वाले बच्चों को फेंक दिया जाता है।
दरअसल बच्चे तो कोई भी अवांछित नहीं होते, न वे नाजायज होते हैं, और न ही हरामजादे या हरामी होते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, और अगर सामाजिक नजरिए से उनके पैदा होने में कोई बुराई है, तो उसके जिम्मेदार उन्हें पैदा करने वाले मां-बाप हैं, या मां अगर अनचाहे गर्भ से लाद दी जाती है, तो बलात्कारी पिता पैदा होने वाले बच्चे के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन इन बच्चों को मारने वाला समाज है। जब कहीं किसी कुंवारी, तलाकशुदा, या विधवा महिला की संतान हो, तो समाज के तमाम ठेकेदार झंडे-डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं कि शादी से परे यह संतान हुई कैसे? समाज का इतना बड़ा दबाव रहता है कि इन तीनों तबकों में से किसी की भी महिला गर्भवती होने के बाद या तो गर्भपात को मजबूर हो जाती है, या फिर बच्चे का जन्म हो जाने पर उसे फेंक देने के लिए। किसी भी मां के लिए नवजात शिशु को फेंक देना आसान नहीं रहता है, क्योंकि उसे नौ महीने पेट के भीतर रखा है, लेकिन समाज की बेरहमी जीना जिस हद तक हराम कर देगी, जितनी सामाजिक प्रताडऩा देगी, उसे झेल पाना हर किसी के लिए आसान नहीं रहता, और समाज की परिभाषा में अवांछित संतान को खुद को भी जिंदगी भर अपने से जुड़े सवालों के जवाब देना आसान नहीं रहता। नतीजा यह रहता है कि नवजात शिशु को फेंक देना कई मुसीबतों का एक इलाज मान लिया जाता है, और एक ताजा-ताजा पैदा हुए बच्चे की जिंदगी का महत्व ही क्या रहता है। अभी-अभी छत्तीसगढ़ में एक हॉस्टल में नाबालिग छात्रा ने वहां शौचालय में एक बच्चे को जन्म दिया, और खुद ही उसे वहां की खिडक़ी से बाहर फेंक दिया। बुरी तरह जख्मी हालत में बच्चे को अस्पताल में बचाने की कोशिश की जा रही है, और इस नाबालिग लडक़ी को जिस परिचित बालिग ने गर्भवती किया था, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
दरअसल समाज में सैकड़ों बरस पहले कुछ जातियों में कुंवारी लडक़ी के मां बनने को उतना बुरा नहीं माना जाता था, और उसकी भी शादी हो जाती थी, और वह साथ में बच्चों को लेकर जाती थी। महाभारत काल के कथानक पर कन्नड़ लेखक भैरप्पा के लिखे उपन्यास ययाति को पढ़ें, तो उसमें इस किस्म की समाज व्यवस्था का जिक्र है, और उस वक्त कुछ समाजों में इसे बुरा माना जाता था कि लडक़ी के गर्भधारण की उम्र आ जाने के बाद भी वह गर्भवती नहीं हो रही है। अब वैसी समाज व्यवस्था बाद के बरसों में किस तरह इतनी कट्टर हो गई कि शादी से परे होने वाले बच्चों को मार डालना ही माताओं के लिए अकेला विकल्प हो गया है। इस नौबत का एक दूसरा इलाज बच्चों को फेंक दिए जाने से बचाकर उन्हें छोड़ दिए जाने का समाधान उपलब्ध कराने वाले अनाथाश्रम थे। मदर टेरेसा की संस्था दशकों से भारत में ऐसे अनाथाश्रम चलाती थीं जहां बाहर रखे झूलों में बच्चों को छोडक़र जाया जा सकता था, और कोई जानकारी नहीं देनी पड़ती थी। अभी हाल के बरसों में ऐसी कई संस्थाओं को विदेशों से दान मिलने में रोक लगने लगी है, और मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी का विदेशी अनुदान पाने का अधिकार रोक दिया गया था, जिसे बाद में वापिस शुरू किया गया। हाल ही में देश में हजारों संस्थाओं के ऐसे पंजीयन रद्द किए गए, लेकिन उनमें से सब अनाथ बच्चों के काम में नहीं लगे हुए थे, वे अलग-अलग कई तरह के सामाजिक काम करते थे।
कुल मिलाकर हम इस बात पर लौटते हैं कि इस देश की बहुत सी धार्मिक, आध्यात्मिक, और सामाजिक संस्थाओं के लिए यह आसान काम हो सकता था कि वे ऐसे अनाथाश्रम शुरू करें जहां लोगों से बिना किसी सवाल-जवाब के अनचाहे बच्चों को लिया जा सके, और उन्हें बच्चों की चाह वाले परिवारों को कानूनी औपचारिकताओं के बाद दिया जा सके। किसी नवजात की जिंदगी ले लेना उसकी मां की क्रूरता कम है, समाज व्यवस्था की क्रूरता अधिक है जो कि ऐेसे मां-बच्चे का जीना हराम कर देती है। लोगों को इसी के बारे में सोचना चाहिए, और किसी उदार संगठन को ऐसे संस्थान शुरू करने चाहिए जहां निजता और गोपनीयता के साथ गर्भवती लड़कियां और महिलाएं जा सकें, वहां सुरक्षित जन्म दे सकें, और फिर अगर उन्हें बच्चों को छोडक़र आना है, तो छोडक़र आ सकें। इससे अजन्मे और नवजात बच्चों के सुरक्षित जिंदगी के अधिकार की गारंटी हो सकेगी। बहुत सी स्थितियों में अकेली लडक़ी और महिला के लिए पूरी गर्भावस्था उसे छुपा पाना आसान नहीं रहता, और न ही जन्म देना और बच्चे को पालना। इसलिए या तो संसद, या कोई सरकार, या कोई अदालत ऐसा इंतजाम करे कि गर्भवती लड़कियों और महिलाओं को बिना किसी भी सवाल-जवाब के, पूरी गोपनीयता के साथ ऐसे संस्थान में दाखिला मिले, और बाद में कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करके उनसे मिले बच्चों को जरूरतमंद परिवारों को दिया जा सके। कोई भी संवेदनशील सरकार आसानी से ऐसा कर सकती है, और यह बहुत महंगा इंतजाम भी नहीं रहेगा। अजन्मे और नवजात इंसानों की जिंदगी बचाना किसी भी जिम्मेदार समाज की एक बुनियादी जिम्मेदारी है, और जो समाज अपने आपको बड़ा गौरवशाली मानता है, उसे नवजात मौतों के ऐसे कलंक से छुटकारा भी पाना चाहिए।
टेक्नॉलॉजी का इतिहास देखें तो उसमें आम लोगों को खास लोगों के मुकाबले कई किस्म से मुकाबले के लायक बनाया है। टेक्नॉलॉजी ने ऐसे कई औजार दिए हैं जिनके बिना विपन्न तबका सम्पन्न तबके का मुकाबला ही नहीं कर सकता था। मशीनों ने रोजगार भी पैदा किए, मजदूरों और कामगारों की उत्पादकता भी बढ़ाई, और लोगों के बीच का फासला घटाया है। एक वक्त था जब सिर्फ सम्पन्न तबके के घर टेलीफोन होता था, और उनके अड़ोस-पड़ोस के किसी व्यक्ति के लिए रिश्तेदार फोन करते थे, तो लोगों को बुलाया जाता था और वे उनके घर बैठकर दुबारा फोन आने का इंतजार करते थे। लोगों के पास घर या दफ्तर-दुकान में फोन होना ताकत और सम्पन्नता का सुबूत था। सम्पन्न लोग काम करते हुए भी अपने घर के लोगों के लिए फोन पर रहते थे, दूसरी तरफ गरीब मजदूर या कामगार घर से निकलने के बाद घर लौट जाने तक संपर्क के बाहर रहते थे। अब मोबाइल फोन की टेक्नॉलॉजी ने शुरूआती एक-दो साल के महंगे रेट के बाद गरीबों के हाथ में एक अभूूतपूर्व और असाधारण ताकत दे दी, और अब लोग झाड़ू लगाते हुए भी, बोरे लादते हुए भी, अपने तमाम करीबी लोगों और रोजगार से जुड़े के लिए उपलब्ध रहते हैं। कामगार के लिए एक काम निपटाते हुए भी अगला काम मौजूद रहता है, और यह मोबाइल फोन की टेक्नॉलॉजी कीमेहरबानी से ही हो पाया है।
ऐसे में टेक्नॉलॉजी ने दुनिया में समानता की एक क्रांति तो लाई है, लेकिन इसके साथ-साथ अब एआई के दाखिले से ऐसा भी लग रहा है कि खर्च करने की ताकत रखने वाला तबका एआई के औजारों का भुगतान करके क्या आगे निकलने की अधिक संभावनाएं खरीद पाएगा? अभी तो एआई खुद अपने शुरूआती दौर में है, और अपने इस्तेमाल करने वाले लोगों से वह लगातार सीख रहा है, और अपने को बेहतर बना रहा है। लेकिन दुनिया भर की कंपनियां जिस अंदाज में आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस में पूंजी निवेश कर रही हैं, उसे कुछ जानकार एक बुलबुला सा मानते हैं जो कि कुछ समय बाद फूट सकता है, और अधिकतर लोगों का पूंजी निवेश डूब भी सकता है। फिर भी निवेशकों का अंदाज यह है कि एआई पर टिकी हुई बहुत से ऐसी चीजें आगे आना बाकी हैं जो कि इस पर काम करने वाली कंपनियों को छप्पर फाडक़र कमाई दे जाएंगी। फिर एआई अपने-आपमें किसी टेक्नॉलॉजी का अंत नहीं है, वह महज पेंट करने के एक ब्रश की तरह है जिससे अलग-अलग कलाकार अलग-अलग पेंटिंग बना सकते हैं, और पिकासो या मकबूल फिदा हुसैन करोड़ों-अरबों कमा सकते हैं। एआई विकसित करने वाले लोग महज ब्रश बनाने वाले लोग हैं। और इसका इस्तेमाल करने वाले लोग पेंटर। अब एआई से कमाई करने के अलग-अलग हजारों किस्म के जरिए हो सकते हैं जिनमें सैकड़ों तो मौजूदा कारोबार की उत्पादकता बढ़ाने वाले, और लागत को घटाने वाले आज भी साबित हो रहे हैं। बीमारियों की शिनाख्त और दवाईयों के आविष्कार का काम एआई की वजह से सैकड़ों गुना तेज हो गया है जो कि बहुत बड़े खर्च को बचा देगा। इस तरह एआई पर आधारित औजार अपने बनाने वाले लोगों का बड़ा फायदा भी करवा सकते हैं, और इस्तेमाल करने वाले लोगों का भी।
लेकिन हमारी एक आशंका यह भी है कि सतह पर तो इससे दुनिया में लोकतंत्र के बढऩे का आसार दिखता है, लेकिन एक खतरा यह दिखता है कि एआई के कई औजार ऐसे भी हो सकते हैं जो कि मोटी रकम से ही खरीदे जा सकें, और उतनी लागत न लगा पाने वाले लोग मुकाबले में पीछे रह जाएं? अगर एआई पर आधारित सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाने वाले लोग कुछ चुनिंदा खरीददारों के हाथों में औजार बन जाएंगे, तो फिर वे इसे न खरीद पाने वाले लोगों के खिलाफ मुकाबले में एक हथियार भी बन जाएंगे। यह कुछ उसी किस्म का हो सकता है कि कुछ छात्रों को कम्प्यूटर और इंटरनेट की सहूलियत हासिल हो, और बाकी तमाम लोग उसके बिना महज किताबों से पढऩे को मजबूर हों। हमारी यह आशंका किसी भी नई टेक्नॉलॉजी के आने, और उसके महंगे रहने तक हर बार रहती आई है। अब एआई चूंकि पिछली हर किस्म की टेक्नॉलॉजी के मुकाबले बिल्कुल अलग किस्म की है, इसलिए इससे संभावनाएं और आशंकाएं भी अलग किस्म की हो सकती हैं। टेक्नॉलॉजी आमतौर पर चीजों को लोकतांत्रिक बनाती है, लेकिन कभी-कभी वह एक गैरबराबरी भी पैदा करती हैं। देखते हैं कि एआई से नफा-नुकसान कितने बरस चलता है, और कब जाकर यह सामाजिक समानता को बढ़ा सकेगी।
अहमदाबाद की एक स्कूल में 8 बरस की बच्ची को गलियारे में चलते हुए कुछ ठीक नहीं लगा तो वह किनारे बेंच पर बैठ गई। उसकी हालत देख उसे पास के अस्पताल में ले जाया गया, तो डॉक्टरों ने उसे दिल के दौरे से मृत बताया। अब 8 बरस की खेलने-खाने की उम्र में एक बच्ची अगर हार्ट अटैक से गुजर जाती है, तो तमाम लोगों को अपने बारे में सोचना चाहिए। अभी कुछ अरसा पहले छत्तीसगढ़ में भी किसी एक जिले में स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगा, तो उसमें कई बच्चों को दिल की बीमारियों की रिपोर्ट निकली। अब अगर ऐसी जांच नहीं हुई होती, तो उन्हें पता भी नहीं लगा होता, और किसी इलाज की संभावना होती, तो वह नहीं हो पाया होता। अब कम से कम उनका इलाज हो सकेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी पुट्टपर्थी वाले सत्य सांई बाबा की संस्था बच्चों के दिल के ऑपरेशन का एक पूरी तरह मुफ्त अस्पताल चलाती है, जहां हर महीने शायद सैकड़ों बच्चों का ऑपरेशन होता है। लेकिन समय पर जांच रहने से कई बीमारियों का इलाज अधिक हद तक, और अधिक आसानी से हो पाता है।
हम यहां लोगों की सेहत से जुड़े हुए दो अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। पहली बात तो यह कि बीमारी की खबर न मिलने पर भी लोगों को अपनी जीवनशैली स्वस्थ रखना चाहिए। आज भारत की बहुत सारी बीमारियां न संक्रामक रोग हैं, और न लोगों को पुरखों से मिली हैं, ये बीमारियां आज की जीवनशैली की वजह से पैदा हुई हैं, या कम से कम पनप रही हैं। एक वक्त डायबिटीज को पैसे वालों की बीमारी माना जाता था, या शहरी जीवनशैली की वजह से यह बढ़ती थी, लेकिन अब तो गांव-गांव तक और गरीबों में भी राजरोग कहा जाने वाला डायबिटीज फैल रहा है, और हिन्दुस्तान को दुनिया का डायबिटीज कैपिटल कहा जा रहा है। दरअसल गांव-गांव तक मजदूरों को भी अब यह आसान लगने लगा है कि बच्चों को कुछ खाने देना हो, तो उन्हें किसी भी दुकान से कोई पैकेट खरीदकर दे दिया जाए, जिसके भीतर का स्वाद बच्चों को बांध लेता है, लेकिन उन्हें ढेर सा नमक, ढेर सी शक्कर, और बहुत सारा फैट दे देता है। शहरी संपन्न बच्चों के इर्द-गिर्द संपन्नता का ऐसा प्रकोप फ्रिज से लेकर अलमारियों तक में भरे रहता है, और कोई रोकटोक मुमकिन नहीं रहती। बच्चों से परे बड़ों का भी यही हाल है, टीवी ने लोगों का उठना और चलना-फिरना भी कम कर दिया है, और मोबाइल फोन से पल भर में हर किस्म के खाने का ऑर्डर करना इतना आसान हो गया है कि लोग रात-दिन अलग-अलग रेस्त्रां के मेन्यू देखकर ऑर्डर करते रहते हैं।
दूसरी तरफ सुबह-शाम सैर या कसरत करना, योग या ध्यान करना, वजन और शुगर लेवल या बीपी को काबू में रखना लोगों को याद ही नहीं रहता। तम्बाकू कई शक्लों में लोगों को कैंसर की तरफ धकेलता है, और लोग इस लत में पडऩे के बाद यह जरूरी भी नहीं समझते कि कैंसर की जांच करवाई जाए, महिलाओं में स्तन और गर्भाशय का कैंसर जिस तरह बढ़ जाने के बाद ही नजर में आता है, उसी तरह अधिकतर मर्दों में तम्बाकू से होने वाला कैंसर हो जाने के बाद ही उनका ध्यान जाता है। इस तरह हिन्दुस्तानी लोगों में न तो बचाव की जागरूकता है, और न ही जांच की। जांच हो जाने के बाद अब इलाज के लिए तो केन्द्र और राज्य सरकारों की कई तरह की बीमा योजनाएं मौजूद हैं, लेकिन वहां तक पहला कदम पहुंचते ही बहुत देर हो चुकी रहती है। चुस्त-दुरूस्त रहकर जिन बीमारियों को टाला जा सकता है, या जिनका खतरा घटाया जा सकता है, उनसे बचने की भी कोई कोशिश अधिकतर लोगों में दिखती नहीं है।
देश को सिर्फ सरकार के कार्यक्रमों से नहीं बचाया जा सकता। सरकार की दी गई सलाह की गंभीरता और विश्वसनीयता दोनों ही सीमित रहती है, और लोगों को लगता है कि उसके पीछे कोई राजनीति है या वोट पाने की कोई नीयत है। इसलिए समाज के दूसरे तबकों से जागरूकता की अधिक जरूरत है, इसे कुछ सामाजिक नेता, और कुछ मशहूर खिलाड़ी या फिल्म सितारे आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी खुद की मिसाल दे सकते हैं, या अखबार और टीवी, या यूट्यूब और वेबसाइटें सेहत के लिए जागरूकता पर कुछ अधिक बात कर सकते हैं। एक और बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि जिस तरह कोई संक्रामक रोग या वायरस लोगों से दूसरे लोगों तक फैलते हैं, उसी तरह सेहत के लिए जागरूकता भी कुछ सेहतमंद और फिट लोगों से दूसरे लोगों तक पहुंचती हैं। ऐसे लोगों की मिसालें भी दूसरों को चौकन्ना करने के काम आ सकती हैं जो उनके आसपास के ही लोग हैं, जिन्हें वे खुद जानते भी हैं। आज हिन्दुस्तान जैसे देश की सरकारें जनता के इलाज पर बहुत सारा खर्च करती हैं, सिर्फ इसे बचाने की नीयत से नहीं, सेहत को कुल जमा बचाने के लिए भी जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए ताकि समय रहते लोग सचेत हो सकें, स्वस्थ जीवनशैली अपना सकें, और फिर भी अगर कोई बीमारी हो, तो उसका वक्त रहते इलाज शुरू करवा सकें। यह चौकन्नापन बचपन से ही जरूरी है, और इसके लिए मां-बाप और परिवार के दूसरे बड़े लोगों को बच्चों के सामने खानपान से लेकर खेलकूद तक भी बेहतर मिसालें पेश करनी होंगी। लोग खुद खराब तौर-तरीके रखें, और बच्चों से बेहतर बनने की उम्मीद करें, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हर किसी को सबसे पहले तो अपनी सेहत और जीवनशैली की फिक्र करनी चाहिए, और इतनी करनी चाहिए कि वे दूसरों के लिए मिसाल भी बन सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने एसटी-एससी आरक्षण के भीतर क्रीमीलेयर को फायदे से बाहर करने पर यह कहा है कि आरक्षण के दायरे से किसी को बाहर करना या न करना, विधायिका और कार्यपालिका का काम है। यह कहते हुए अदालत ने एक जनहित याचिका पर सरकार को कोई आदेश देने से इंकार कर दिया। जस्टिस बी.आर.गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने छह महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की संविधान पीठ के फैसले का जिक्र किया जिसने एसटी-एससी आरक्षण के भीतर उपजातियों के आधार पर और आरक्षण करने को सही ठहराया था। इस फैसले के वक्त के चीफ जस्टिस डी.वाई.चन्द्रचूड़ की अगुवाई में सात में से छह जजों ने इस पर सहमति जताई थी, और एक अकेली जज जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इससे असहमति का अलग फैसला लिखा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी ताजा मामला छह महीने पहले के फैसले के खिलाफ नहीं था, बल्कि एसटी-एससी तबकों के भीतर क्रीमीलेयर को आरक्षण के फायदों से हटाने के बारे में था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से मना कर दिया है लेकिन कहा है कि संविधानपीठ ने सरकार और संसद के सामने यह विचार रखा था कि एसटी-एससी तबकों के भीतर जो लोग पहले से आरक्षण पाते आ रहे हैं, या जो लोग बेहतर स्थिति में हैं, और ताकतवर हो चुके हैं, उन्हें आरक्षण के फायदे से बाहर करने के बारे में विचार किया जाना चाहिए। इस जनहित याचिका पर जजों ने यही याद दिलाया कि उन्होंने पिछले फैसले में यही राय रखी थी, और इस पर कोई कार्रवाई करना सरकार और संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है।
हम सुप्रीम कोर्ट जजों की इस व्याख्या से सहमत नहीं हैं कि अदालत को इस पर विचार नहीं करना चाहिए। जैसा कि अभी की जनहित याचिका के वकील ने सरकार को याद दिलाया कि संविधानपीठ का फैसला आए छह महीने हो चुके हैं लेकिन केन्द्र सरकार ने उस पर विचार करने की भी जहमत नहीं उठाई, और संसद के सामने तो वह मुद्दा है ही नहीं। ऐसे में भारत के राजनीतिक दलों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे एसटी-एससी की क्रीमीलेयर को आरक्षण के फायदों से बाहर करें, या कि आरक्षण का फायदा पाने वाले लोगों की अगली पीढ़ी को इस फायदे से बाहर करें। अदालत को इस बारे में सोचना चाहिए था क्योंकि संसद का काम तो आरक्षण को तय करना है, और आरक्षित तबकों के भीतर अगर कमजोर तबकों के लोग अपने आरक्षित वर्ग के लिए रखी गई सीटों पर मुकाबले के लायक भी तैयार नहीं हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग पीढ़ी-दर-पीढ़ी सिर्फ जाति के आधार पर यह आरक्षण पाते चल रहे हैं, और उन परिवारों की ताकत ऐसे हर फायदे के बाद अगली पीढिय़ों के लिए बढ़ती चल रही है, तो आरक्षित सीटों पर उस वर्ग के सबसे ताकतवर, सबसे संपन्न परिवारों का एकाधिकार सा हो गया है।
हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हम दशकों से इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं कि एसटी-एससी के भीतर भी क्रीमीलेयर तय की जानी चाहिए, ताकि ताकत के ओहदों, और संपन्नता पा लेने वाले लोगों को आरक्षण से बाहर किया जा सके, और उसी समुदाय के उनसे कमजोर लोगों को मुकाबले में खड़े होने का एक मौका दिया जा सके। यह सोच सुप्रीम कोर्ट से लेकर भारत सरकार तक, और संसद से विधानसभाओं तक इसलिए महत्व नहीं पाती है क्योंकि फैसला लेने वाले तमाम लोगों के बच्चे इसकी वजह से आरक्षण के फायदों से बाहर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज, अखिल भारतीय सेवाओं के अफसर, सांसद और विधायक, और संपन्न लोग, ये सब लोग क्रीमीलेयर में आएंगे, और भला इनमें से कौन अपने बच्चों को आरक्षण के फायदों से दूर करना चाहेंगे। यह सिलसिला तोडऩे के लिए एक जनमत और जनआंदोलन जरूरी है जो कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, और विधायिका सभी को यह अहसास कराए कि उसमें निर्णायक कुर्सियों पर बैठे हुए लोग अपने बच्चों के फायदे जारी रखने के लिए एसटी-एससी के भीतर क्रीमीलेयर लागू नहीं होने देना चाहते हैं। हमारा साफ मानना है कि यह निर्णायक तबके के हितों के टकराव का मामला है, और इसीलिए अदालत, सरकार, और संसद, कोई भी यह आत्मघाती फैसला लेना नहीं चाहते हैं जो कि इन आरक्षित वर्गों के कमजोर लोगों के लिए जरूरी है। एसटी-एससी तबकों में भी यह जागरूकता जरूरी है कि उनके सबसे ताकतवर लोग आरक्षण का सारा फायदा खा जा रहे हैं। जब तक इन तबकों का बहुमत जागरूक नहीं होगा, तब तक इन तबकों के मुखिया लोग तीनों लोकतांत्रिक संस्थाओं पर काबिज रहकर अपने ही बच्चों को बचाने में लगे रहेंगे।
आज दिक्कत यह है कि एसटी-एससी तबकों के जो मुखिया हैं, वे भी कहीं न कहीं क्रीमीलेयर जितनी ताकत और संपन्नता पा चुके हैं, और इसीलिए वे जरा भी जागरूकता नहीं आने देना चाहते। देश को ऐसी तंगदिली, और ऐसी तंगनजर से उबरने की जरूरत है, कहने के लिए तो तीनों लोकतांत्रिक स्तंभों के मुखिया लगातार अपने को समाजकल्याण में लगा हुआ बताते हैं, लेकिन एसटी-एससी के सचमुच कमजोर लोगों के साथ पौन सदी से जो बेइंसाफी चली आ रही है, वह दूर करने में इनमें से किसी की दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं के परिवारों के पेट पर लात पड़ेगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को सुनने से मना कर दिया है, तो अब जनजागरण के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और लोगों को संसद और विधानसभा से लेकर, स्कूल-कॉलेज तक, सरकारी नौकरियों तक, और म्युनिसिपल-पंचायत चुनावों तक क्रीमीलेयर को मुद्दा बनाना चाहिए, इस लोकतंत्र में इंसाफ पाने के लिए जनजागरूकता, और जनआंदोलन ही असरदार हो सकते हैं।
पुलिस के रोज के प्रेसनोट हत्या या बलात्कार के जुर्म में पकड़े गए लोगों से लेकर मामूली उठाईगिरी तक के मामलों में पकड़ाए आरोपियों की तस्वीरों सहित रहते हैं। कुछ मामले तो सुबूतों सहित पकड़ाते हैं, और पहली नजर में आरोपियों के गुनहगार होने की बात सही लगती है, लेकिन बहुत से ऐसे मामले रहते हैं जो सिर्फ किसी के लगाए गए आरोपों पर टिके रहते हैं। और कई मामलों में तो यह भी सामने आता है कि बलात्कार का आरोप लगाने वाली लडक़ी या महिला ने बाद में आरोप वापिस ले लिए, और ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। अभी-अभी ऐसी ही एक महिला को उसके तीन-चार साथियों सहित गिरफ्तार किया गया है जो कि एक कारोबारी पर बलात्कार का आरोप लगाने के बाद, उसके जेल जाने के बाद शिकायत वापिस लेने के लिए मोटी वसूली कर रही थी। ऐसे में क्या पहली शिकायत के बाद ही आरोपियों की तस्वीर जारी करना ठीक है? भारत की अदालतों में हाईकोर्ट तक पहुंचते हुए शायद आधे से अधिक मामलों में लोग बरी हो जाते हैं। ऐसे में उनकी तस्वीर, या उनकी शिनाख्त की खबर से उन्हें हुए नुकसान की कोई भरपाई हो सकती है क्या? और भारतीय कानून क्या अदालती सजा से परे सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की किसी और सजा सुझाता है?
अभी उत्तरप्रदेश के झांसी में पुलिस ने गश्त के दौरान एक ऐसे आदमी को पकड़ा जिसकी बिहार में 17 बरस पहले हत्या दर्ज हो चुकी है, और उसका कत्ल करने के आरोप में चार लोगों को जेल भी हो चुकी है जिनमें से तीन अभी जमानत पर छूटे हुए हैं, और एक व्यक्ति कत्ल की तोहमत झेलते हुए मर भी चुका है। जब इसने झांसी पुलिस को अपनी शिनाख्त बताई, तो उसने बिहार पुलिस को बुलाकर इस आदमी को उनके हवाले किया, और तब पूरा मामला पता लगा कि वह 2008 से बिहार के अपने गांव से निकल गया था, और फिर कभी गांव लौटा नहीं। इसके बाद जिन लोगों के खिलाफ शक के आधार पर अपहरण और हत्या की रिपोर्ट लिखाई गई, उन्हें गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया, और 8-8 महीने जेल में रहने के बाद वे जमानत पर छूटे, और हिन्दुस्तानी अदालती रफ्तार की मेहरबानी से 17 बरस बाद भी जो रिश्तेदार हत्या की तोहमत झेल रहे थे, उन्हें कोई सजा नहीं हो पाई थी, वरना पता लगता कि कुछ लोग फांसी पर टंग चुके रहते। पारिवारिक रिश्तेदारी में ही 17 बरस से कत्ल की तोहमत झेल रहे इन लोगों पर क्या गुजर रही होगी, उसे वे ही जानते हैं।
अब अगर आज की तरह ही उस वक्त पुलिस ने प्रेसनोट में इन चारों आरोपियों की तस्वीरें जारी की होंगी, तो उनके चेहरों के साथ उनकी बदनामी कदमताल करते हुए चलती होगी। वैसे भी नाम तो उनका जारी हो ही चुका होगा। अब अगर अखबारों से इस बारे में पूछा जाए तो वे तो बिना ऐसे चेहरे और ऐसी तस्वीरों के खबर ही नहीं बना सकते। उन्हें लगेगा कि मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट से होने के पहले तक तो कोई भी व्यक्ति अंतिम रूप से मुजरिम साबित नहीं होता, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले, या वहां पर अपील करने का वक्त निकल जाने के बाद ही समाचार बनाया जाए? खबरों के पेशे के लिए तो यह सवाल जायज है, लेकिन जब कानून किसी को मुजरिम नहीं मानता, और महज आरोपी या अभियुक्त मानता है, और मुकदमा चलाते रहता है जो कि 25-30 बरस तक चलना भी हो सकता है, तो फिर बेकसूर साबित होने पर ऐसी बदनामी की क्या भरपाई हो सकती है?
दुनिया में जो अधिक संवेदनशील लोकतंत्र हैं, वहां पर भी आरोपियों के मुजरिम साबित होने के पहले भी उनकी फोटो और जानकारी छापना आम बात है। लेकिन एक बुनियादी सवाल बचे रहता है कि कानून बदनामी करने की सजा तो देता नहीं है, किसी के मुजरिम साबित होने के पहले तक तो उसे बेगुनाह साबित होने का पूरा हक रहता है, जो कि खबरों में आई बदनामी से खत्म होता है। ऐसे में किसी मामले में झूठी शिकायत, गलतफहमी, या सुबूतों की गफलत से पकड़ में आए लोगों के साथ इंसाफ कैसे हो सकता है? भारत जैसे कानून में सिर्फ कुछ लोगों को इससे छूट हासिल है, जो नाबालिग किसी भी किस्म के जुर्म के मामलों में फंसते हैं, उनका नाम, या किसी भी तरह की शिनाख्त उजागर नहीं हो सकते। इसी तरह सेक्स अपराधों की शिकार लडक़ी या महिला की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। लेकिन इससे परे तो सभी तरह के लोग बदनामी पाने से शुरूआत करते हैं, और असल सजा होने तक तो वे सामाजिक प्रताडऩा की सजा पूरी तरह झेल चुके रहते हैं, और उनका परिवार भी इसका नुकसान पा चुका रहता है।
इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा मुद्दा बेकसूर लोगों का है जो कि लंबी बदनामी, और लंबी कैद, सुनवाई के बाद सब कुछ खोकर बेकसूर साबित होते हैं, और उसके बाद उनकी जिंदगी वापिस कभी पटरी पर आ भी नहीं पाती। भारत में आतंक जैसे गंभीर आरोपों में जेलों में कैद लोग 20-25 बरस बाद भी छूटे हैं, तो उसके बाद बाहर की दुनिया मानो उनके लायक रह ही नहीं जाती। यह मामला आरोपियों के मीडिया कवरेज से कुछ परे का है, लेकिन बेइंसाफी तकरीबन एक किस्म की है। एक मामले पर गौर करना जरूरी है कि हिन्दुस्तान में बच्चों से बलात्कार, उनका कत्ल, और उनकी लाश के टुकड़े पकाकर खाना जैसे भयानक आरोपों वाले सबसे चर्चित 2006 के निठारी हत्याकांड के आरोपियों को अभी 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सारे जुर्मों से बरी कर दिया है। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी, और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट भी गई है जहां अभी उस पर सुनवाई होनी है। अब सवाल यह उठता है कि इतने बरस तक जिन लोगों को हैवान और पिशाच कहा जाता रहा, और अब हाईकोर्ट अगर उनको बेकसूर मान चुका है, सुप्रीम कोर्ट अगर बेकसूर करार दे देता है, तो इतने बरस की बदनामी, या जितने भी बरस की कैद रही हो, उसकी क्या भरपाई हो सकती है?
अब हमारे सवालों के जवाब में हमारे पास कहने को कुछ भी नहीं है कि लोकतंत्र में जनता को अपने बीच के जुर्म के आरोपियों के बारे में जानने का कितना हक होना चाहिए, और उन आरोपियों को अपनी निजता का, और सामाजिक प्रतिष्ठा का कितना हक होना चाहिए? बदनामी करने का पुलिस और मीडिया का कितना हक हो, और वह कब से शुरू हो? ये मुश्किल सवाल हैं, और लाजवाब भी हैं। देखें क्या किसी के पास इस दिक्कत का कोई इलाज निकल सकता है?
फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा ने अमरीका में फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम बंद करने का ऐलान किया है। अब तक भारी सार्वजनिक और अमरीकी-संसदीय दबाव के तहत दुनिया की यह सबसे चर्चित कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर आने वाली सामग्री में सच-झूठ, अफवाह, और नफरत, इसकी सच्चाई की कुछ जांच-पड़ताल करती थी। जबकि हिन्दुस्तान में हमारे सरीखे लोगों का यह तजुर्बा रहा कि इस पर लगातार नफरती फोटो-वीडियो, या दूसरी सामग्री पोस्ट होती रहती थी, होती रहती है, और यहां कंपनी कोई जवाबदेही भी नहीं मानती। और तो और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर लगातार पूरी तरह से फर्जी और धोखेबाज विज्ञापन आते रहते हैं, और कंपनी उनको रोकने की जहमत भी नहीं उठाती, जबकि उन विज्ञापनों का पैसा लेते हुए कंपनी की नजर में वे अलग से आते ही हैं, वे लोगों की निजी फोटो, कविता, या किसी टिप्पणी से परे की ठोस बात रहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि फेसबुक को उनसे कमाई होती है।
लोगों को मुफ्त में सोशल मीडिया की सहूलियत मुहैया कराने के बाद ये कंपनी उनकी मौजूदगी का नगदीकरण करती हैं। अमरीका और योरप, जहां पर कि कानून कड़े हैं, उन पर अमल अधिक सख्त है, वहां पर तो फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ जिम्मेदारी दिखाते भी हैं क्योंकि अमरीकी संसद की समिति की सुनवाई में मार्क जुकरबर्ग को खुद पेश होकर सांसदों के हर सवालों का जवाब देना पड़ा था, और सांसदों ने मानो बंदूक की नोंक पर जुकरबर्ग को खड़ा करके उन लोगों से माफी मंगवाई थी जिनके बच्चों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम सरीखे प्लेटफॉर्म की वजह से खुदकुशी कर ली थी। इस सुनवाई का जीवंत प्रसारण भी हुआ था, और यह देखना बड़ा दिलचस्प था कि दुनिया के एक सबसे ताकतवर आदमी को अमरीकी संसद की कमेटी किस तरह बांह मरोडक़र दुखी मां-बाप के सामने खड़े होकर माफी मांगने को मजबूर करती है। यूरोपीय संघ जैसे ताकतवर संगठन भी फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने नियम, और अपनी शर्तें लागू करते हैं, और ऐसे विकसित, सभ्य, ताकतवर, और जागरूक देशों के सामने मेटा जैसी कंपनियां भीगी बिल्ली की तरह सहमी हुई खड़ी रहती हैं।
अभी अमरीका में फैक्ट चेक बंद करने के पीछे मार्क जुकरबर्ग ने तर्क दिया है कि कंपनी के बाहर के फैक्ट चेकर्स ने राजनीतिक पक्षपात किया था, उससे फेसबुक इस्तेमाल करने वालों का भरोसा टूटा है। उनका तर्क यह है कि तथ्यों की जांच करने से जितना भरोसा बनना था, उससे अधिक टूट गया है। हकीकत तो यह है कि अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव में जिस तरह से डोनल्ड ट्रम्प जीतकर आए हैं, और जिस तरह से एक बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ट्रम्प के सबसे बड़े सलाहकार और मददगार बनकर साथ खड़े हुए हैं, इन दोनों की जोड़ी को देखकर अमरीकी कारोबारी रंग बदल रहे हैं। अभी-अभी मेटा ने ट्रम्प के एक बहुत करीबी व्यक्ति को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मनोनीत भी कर लिया है। और सच के लिए न ट्रम्प के मन में कोई भरोसा रहा, न एलन मस्क के। जब मस्क ने ट्विटर खरीदा था, तब से लेकर उसे एक्स बनाने तक मस्क लगातार किसी भी तरह की जांच-पड़ताल के खिलाफ रहे, और अराजकता की हद तक लोगों के पोस्ट करने के हिमायती रहे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर एलन मस्क ने किसी भी तरह के झूठ को, नफरत, और हिंसा को ट्विटर से हटाने से मना कर दिया था। यह सारा सिलसिला उनके पसंदीदा राष्ट्रपति पद प्रत्याशी डोनल्ड ट्रम्प की सहूलियत का था जो कि अमरीकी वोटरों के सामने तरह-तरह से झूठ परोसकर, उन्हें बरगलाकर चुनाव जीतने की तरफ बढ़ रहे थे। अब मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने यह साबित कर दिया है कि अमरीकी कारोबारी दुनिया में जिधर बम, उधर हम की नीति ही काम करती है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह एक निर्वाचित अमरीकी राष्ट्रपति काम संभालने के महीनों पहले से दुनिया के सबसे रईस आदमी, और अमरीका के एक सबसे बड़े कारोबारी एलन मस्क की तय की हुई राह पर चल रहा है, मस्क के लिए हुए फैसलों पर हामी भरने से परे उसका कोई काम नहीं है। ऐसे में ट्रम्प और मस्क को सख्त नापसंद, झूठ और सच की जांच-पड़ताल को मेटा ने कचरे के ढेर पर डाल दिया है। अब दिखावे के लिए वहां कोई और तरीका ईजाद करने की बात कही जा रही है, लेकिन अब वहां झूठ को रोकने का एक योजनाबद्ध और संगठित तरीका खत्म कर दिया गया है।
हिन्दुस्तान जैसे देश को यह सोचना चाहिए कि क्या फेसबुक का ऐसा मॉडल भारत को भी मंजूर रहेगा, या फिर भारत अपनी कुछ शर्तें भी फेसबुक पर लगा सकता है? हम ऐसी सलाह तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह की रोकटोक का हक सरकार को तानाशाही की तरफ बढ़ाता है, और सरकारों को अधिक अधिकार दिए नहीं जाने चाहिए। फिर भी अगर कोई सर्वदलीय संसदीय समिति ऐसी बन सकती है जो कि आज जिंदगी पर सबसे अधिक असर डालने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय कर सके, तो वैसी कोशिश जरूर करनी चाहिए। भारत की पहले से लदी हुई अदालतों पर सोशल मीडिया के झूठ और नफरत का बोझ और नहीं लादा जा सकता। इसके बारे में संसद को ही सोचना होगा, और किसी तरह की सेंसरशिप के बजाय संसदशिप जैसा एक अधिकार लागू करना होगा, ताकि देश किसी एक राजनीतिक विचारधारा के मुताबिक काबू लागू न करे, और जनहित में विचारधाराओं का एक अधिक विविध मंच सोशल मीडिया की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करे।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बड़े नक्सल हमले में सडक़ पर लगाए गए विस्फोटक से पुलिस की गाड़ी उड़ा दी गई, और 8 जवानों के साथ एक गैरपुलिस ड्राइवर की जान चली गई। सुरक्षाबलों की ऐसी शहादत करीब दो बरस बाद हुई है, उसकी एक वजह शायद यह भी है कि इस बीच विधानसभा और लोकसभा चुनावों के चलते महीनों तक बस्तर में बाहर से भेजे गए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती थी, और चौकसी भी अधिक थी। एक तरफ तो पिछले 12 महीनों में छत्तीसगढ़ की भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार ने लगातार नक्सल मोर्चे पर अभूतपूर्व और असाधारण कामयाबी पाई है, और 287 नक्सली एक कैलेंडर वर्ष 2024 में ही मारे गए, जिनमें से कुछ के आम आदिवासी ग्रामीण होने के आरोप भी लगे थे, लेकिन उनकी गिनती हाथ की उंगलियों से अधिक नहीं थी। इस एक बरस में नक्सल हिंसा से घिरे बस्तर में मानवाधिकार हनन के मामले भी बीते बरसों के मुकाबले बहुत कम हुए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस सरकार ने अपने पहले बरस में ही पिछली कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के आखिरी बरस के 20 नक्सलियों को मारने की संख्या से 12-14 गुना अधिक का एक रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन नए साल के पहले हफ्ते में ही पुलिस का यह एक बड़ा नुकसान हुआ है जब सडक़ पर लगाए गए किसी बहुत बड़े विस्फोटक से पुलिस गाड़ी को उड़ाया गया, उसके चिथड़े उड़ गए, और टुकड़े-टुकड़े दूर-दूर तक पेड़ों पर टंगे हुए मिले।
इसे सुरक्षाबलों की बहुत बड़ी शिकस्त की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक बड़े नुकसान की तरह देखना चाहिए। जिस तरह 50-60 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मी बस्तर के नक्सल मोर्चे पर तैनात हैं, और उनके 10 फीसदी से भी कम नक्सली वहां लगातार नुकसान झेल रहे हैं, वह कुल मिलाकर तो सुरक्षाबलों की कामयाबी का एक बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन हथियारबंद टकराव और फौजी कार्रवाई के किसी भी इलाके में अलग-अलग वक्त पर इस तरह का कोई अकेला हमला दूसरे खेमे की कई जिंदगियां ले सकता है। जब तक हथियारबंद संघर्ष जारी रहता है तब तक दोनों तरफ की वर्दियों की जिंदगियों की कोई गारंटी नहीं रहती है। प्रदेश की भाजपा सरकार के गृहमंत्री विजय शर्मा ने साल भर पहले से जिस जोर-शोर से नक्सलियों से बातचीत की घोषणा की थी, वह शुरू होने की कोई सुगबुगाहट भी नहीं दिख रही है। ऐसे में बस्तर में जिंदगियां हमेशा ही खतरे में बनी रहेंगी। यह जरूर है कि पिछले एक साल में लगातार बढ़ी हुई सुरक्षाबलों की मौजूदगी, और उनके कामयाब ऑपरेशनों के चलते नक्सली बहुत कमजोर हुए हैं, उनके बहुत से लोग मारे गए हैं, लेकिन इसके लिए जितनी बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती करनी पड़ी है, उस पर जो दानवाकार खर्च हमेशा से होते आया है, उन सबको देखते हुए, और कल का जिंदगियों का यह नुकसान देखते हुए एक बार फिर लगता है कि गोलियों के अलावा बातचीत की कोशिश भी करनी चाहिए। यह तो ठीक है कि सुरक्षा कर्मचारी सरकार के हुक्म पर कितने भी खतरे उठाने के लिए तैयार या मजबूर रहते हैं, लेकिन इन खतरों को किसी तरह से अगर कम किया जा सके, तो उसकी कोशिश भी कम अहमियत नहीं रखती है। पिछले एक साल में अगर बातचीत शुरू होकर किसी भी कामयाबी तक पहुंचती, तो इंसानी जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान टल सकता था। नक्सली भी इसी देश के नागरिक हैं, और अगर उन्हें समझाकर हिंसा से दूर किया जा सकता, तो दोनों तरफ की करीब तीन सौ जिंदगियां बच सकती थीं। लोकतंत्र में ऐसे बागियों, विद्रोहियों, या उग्रवादियों, आतंकवादियों को भी कानून के तहत जीने को तैयार करना लोकतांत्रिक ताकतों की कामयाबी भी होती है, और जिम्मेदारी भी होती है। हथियारबंद समूह तो लोकतंत्र पर भरोसा करते नहीं हैं, इसलिए वे लोकतंत्र से परे रहते हैं, उनसे संविधान पर भरोसे की उम्मीद नहीं की जा सकती, उन्हें इसके लिए सहमत जरूर कराया जा सकता है, और पूरी दुनिया में हथियारबंद उग्रवाद से निपटने में बिना बातचीत कामयाबी मिली भी नहीं है। खुद हिन्दुस्तान में पंजाब से लेकर उत्तर-पूर्वी प्रदेशों तक बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि बातचीत से सशस्त्र संघर्ष खत्म हुए हैं, और कल के उग्रवादी आज लोकतांत्रिक चुनावों की मूलधारा में आकर कानून के तहत काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं।
दरअसल देश-प्रदेश की राजधानियों में बसे हुए शहरी लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि गोली का जवाब गोली होना चाहिए। लेकिन ऐसा जवाब देते हुए बेकसूर सुरक्षाकर्मियों की शहादत भी होती है। यह मानकर चलना ठीक नहीं है कि राज्य पुलिस या केन्द्रीय सुरक्षाबलों में जो लोग नौकरी पर आते हैं, उन्हें जान और शहादत देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऐसे नुकसान को हमेशा एक आखिरी और तकलीफदेह विकल्प की तरह मानना चाहिए, और उससे बचने की हर कोशिश करनी चाहिए। बातचीत का महत्व हम इसलिए भी अधिक आंकते हैं कि बंदूकों की कार्रवाई के शहरी और राजधानीनिवासी लोगों की अपनी जिंदगी इन जंगलों में दांव पर नहीं लगी रहती है। नक्सलियों की तरह के जो लोग भारत के संविधान के खिलाफ बंदूक का राज चाहते हैं, उन्हें बंदूक से जवाब देना तो ठीक है, लेकिन वह लोकतंत्र की सबसे अच्छी किस्म की कामयाबी नहीं है।
बस्तर का कल का नक्सल हमला यही साबित करता है कि एक बरस में उनका नुकसान चाहे जितना हो गया हो, वे गिनती में चाहे कितने ही कम क्यों न रह गए हों, सुरक्षाबल चाहे कितने ही बढ़ क्यों न गए हों, जब तक नक्सल हिंसा पूरी तरह खत्म नहीं होती है, सुरक्षा कर्मचारियों और बस्तर के आम नागरिकों पर ऐसा खतरा बने ही रहेगा। सरकार कानूनसम्मत जो भी कार्रवाई करे वह तो ठीक है, लेकिन बातचीत के महत्व को पूरी तरह भुला देना ठीक नहीं है। यह भी हो सकता है कि बातचीत की सलाह को कई लोग एक अर्बन-नक्सल सलाह मान लें, लेकिन उसी गलतफहमी को दूर करने के लिए हम याद दिलाना चाहेंगे कि अभी साल भर के भीतर ही प्रदेश के गृहमंत्री ने बार-बार बातचीत पर जोर दिया था, और यह तक कहा था कि उनसे वीडियो कॉल करके भी नक्सली शांतिवार्ता कर सकते हैं। सरकार को ऐसी बातचीत का कोई रास्ता निकालना चाहिए, प्रदेश के भीतर या बाहर कुछ ऐसे मध्यस्थ हो सकते हैं जो कि नक्सलियों को बातचीत के लिए सहमत कर सकें। प्रदेश और देश से नक्सलियों को खत्म करने के लिए उन सबकी लाशें गिराने से बेहतर रास्ता उन्हें हिंसा और बंदूक छोडऩे के लिए तैयार करने का होगा। जब तक वे रहेंगे, बीच-बीच में अगर इसी तरह के हमलों में कई जिंदगियां चली जाएंगी, तो इससे राजधानियों का तो नुकसान नहीं होगा, देश-प्रदेश के अलग-अलग गांव-कस्बों में बसे हुए उन दुखी परिवारों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसे परिवारों की तकलीफ देखकर सरकार को शांतिवार्ता की अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी भी पूरी करनी चाहिए, ताकि जिंदगियां बचाई जा सकें। हम कल की घटना के पीछे सुरक्षाबलों की किसी चूक या लापरवाही की बात करना नहीं चाहते, लड़ाई के मैदान में कभी न कभी ऐसी चूक होती है, और कभी न कभी कमजोर पक्ष को भी वार करने का मौका मिल जाता है। इससे सबक जरूर लिया जा सकता है, लेकिन हिंसा पूरी तरह से खत्म तो राजधानियों में बातचीत की टेबिलों पर ही होगी।
महाकुंभ मेले को नासर पठान नाम की एक आईडी से सोशल मीडिया पर धमकी दी गई कि कुंभ में एक विस्फोट से कम से कम हजार लोगों को मार डाला जाएगा। इस आईडी को नासर कट्टर मियां भी लिखा गया, और इससे होने वाली पोस्ट में इंशा अल्लाह और अल्लाह इज ग्रेट जैसे शब्दों के साथ विस्फोट में हजार से अधिक को मारने की बात लिखकर सनसनी फैला दी गई। कुंभ को लेकर यूपी पुलिस कुछ चौकन्ना चल रही है क्योंकि कनाडा में बसे खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी कुंभ पर कुछ खास पर्वों के दिन खालिस्तानी हमले की धमकी दी है। अब वह धमकी तो चाहे जैसी भी रही हो, भारत में आज हिन्दू-मुस्लिम तनाव एक बड़ा मुद्दा है, और इसलिए यूपी पुलिस ने बहुत तेजी से इस सोशल मीडिया अकाउंट की तह तक पहुंचकर धमकी पोस्ट करने वाले को गिरफ्तार किया। हजार लोगों को मार डालने की धमकी नासर पठान के नाम से पोस्ट करने वाला बिहार का नौजवान आयुष कुमार जायसवाल निकला। उसने एक मुस्लिम नाम से फर्जी आईडी बनाई थी, और यह सनसनी, नफरत, और साम्प्रदायिकता फैलाने का काम किया था। 31 दिसंबर को यह पोस्ट करने के बाद आयुष नेपाल चले गया था, और अब पुलिस उसके नेपाल कनेक्शन भी तलाश रही है।
अब कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला होने जा रहा है, जिसमें डेढ़ महीने में 40 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। हिन्दू आस्था का यह प्रदर्शन केन्द्र और राज्य सरकार की तरह-तरह की आर्थिक मदद से हो रहा है, और सरकार ही इसमें मेजबान भी है। देश भर के हिन्दुओं को इसके लिए न्यौता दिया जा रहा है, और कुछ खास दिनों पर तो यहां एक दिन में एक करोड़ से अधिक लोगों के भी आने की उम्मीद है। जहां धार्मिक वातावरण में इतने लोग एकजुट होने हों, उस आयोजन को लेकर वहां पहुंचने वाले लोगों के बीच एक मुस्लिम के नाम से विस्फोट से कम से कम हजार लोगों को मार डालने की धमकी देने की कई तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है। इतनी भीड़ के बीच किसी फेरीवाले मुस्लिम को लेकर अगर लोगों को कोई शक हुआ, और उसे घेरकर मार डाला गया, तो वैसे तनाव के पीछे इस फर्जी पोस्ट से शुरू साम्प्रदायिकता भी जिम्मेदार रहेगी। आज देश भर में जगह-जगह धर्मान्ध भीड़ किसी को भी घेरकर मार रही है, और वैसे में कुंभ को लेकर इस तरह की साम्प्रदायिक धमकी देना देश में दंगा फैलाने की हरकत से कम कुछ नहीं है।
अब सोशल मीडिया और मैसेंजर सर्विसों की मेहरबानी से लोगों को सुबह चाय का पहला कप मिलता है, उसके पहले वे हजार-पांच सौ लोगों के बीच नफरत बांट चुके रहते हैं। फिर जिन्हें नफरत के ऐसे झूठे वीडियो और गढ़े हुए पोस्ट मिलते हैं, वे इसे अपनी सार्वजनिक, राजनीतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी मानते हुए और लोगों को आगे बढ़ा देते हैं। यह देश ऐसी सोच पर खड़ा हुआ है जिसमें किसी देवी से लेकर सांई बाबा तक के पर्चों को बांटने के काम में लोग जुट जाते हैं, क्योंकि 21 लोगों तक वैसा पर्चा लिखकर न बांटने से बड़ा अशुभ हो सकता है, ऐसी मजबूत सोच इस देश के लोगों की है। इसलिए खासे पढ़े-लिखे और वैज्ञानिक जानकारी के लोग नफरत फैलाने के लिए मानो सुबह अलार्म लगाकर जल्दी उठते हैं कि मुर्गा लोगों को जगा सके उसके पहले वे लोगों के भीतर नफरत को जगाने में कामयाब हो चुके रहें। ऐसे लोगों के हाथ जब नासर पठान के नाम से जारी ऐसी धमकी मिलती है जो कि हिन्दुओं के सबसे बड़े आस्था-मेले में आतंकी हमले की बात करती है, तो जाहिर है कि इसे भी आगे बढ़ाया जाएगा, बढ़ाया जा चुका होगा। और पुलिस ने जांच में नासर पठान की जगह आयुष जायसवाल को पाया है, इस बात को नफरतियों की दस फीसदी भीड़ भी आगे नहीं बढ़ाएगी। इसलिए झूठ जब चारों तरफ आग लगा चुका रहता है, सच एक बाल्टी रेत लेकर सोचता है कि बुझाना कहां से शुरू किया जाए।
हमारा मानना है कि बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने की ऐसी साजिश करने वाले लोगों को किसी स्पेशल कोर्ट के तहत तेजी से सजा मिले, और बाकी लोगों को सबक मिले। अभी तो हम नफरत फैलाने वालों को कोई सजा मिलना तो दूर, कोई समन मिलते भी नहीं देखते। जाहिर है कि ऐसे में सबके हौसले बढ़ते चलते हैं, और देश के अधिकतर हिस्सों में बहुसंख्यक धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक धर्म के लोगों के हक पर आपत्ति होने लगी है। यह पहला ऐसा मौका नहीं है कि यूपी-बिहार जैसे हिन्दीभाषी, हिन्दू बहुतायत वाले प्रदेशों में ऐसी हरकत की गई हो। पिछले बरस यूपी में एक थानेदार का तबादला करवाने के लिए उस इलाके के कुछ हिन्दू गुंडों ने गाय कटवाकर कुछ जगहों पर फेंक दी, और उसके पास एक मुस्लिम का परिचय पत्र डाल दिया था ताकि साम्प्रदायिक दंगा हो जाए तो थानेदार का तबादला हो जाएगा। बाद में सीएम योगी की पुलिस के एक हिन्दू आईजी के मातहत एक हिन्दू एसपी के मातहत कई दूसरे हिन्दू अफसरों ने मिलकर गाय कटवाने वाले इन हिन्दुओं को गिरफ्तार किया था। अब यह कल्पना की जा सकती है कि अगर कोई साम्प्रदायिक दंगा हो गया रहता तो वह कहां-कहां तक फैलता, और बाकी देश में भी उसकी चिंगारियां पहुंचतीं।
हिन्दुस्तान के बहुत से लोगों की धार्मिक भावनाओं को बड़ी कोशिश करके बारूद के ढेर पर बिठाकर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट कभी इस साजिश को समझने का दिखावा करता है, और पूरे देश के लिए बार-बार कड़े हुक्म देता है कि हेट स्पीच पर अफसर तुरंत खुद ही जुर्म दर्ज करें, किसी शिकायत का इंतजार न करें, वरना उन्हें सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया जाएगा। लेकिन इस पर अमल कहीं भी नहीं दिखता है। नफरत के ऐसे माहौल में, बारूद के ऐसे ढेरों के इर्द-गिर्द नफरती आतिशबाजी करने में लगे हुए लोगों को मामूली कानून में सजा देना काफी नहीं होगा। इन्हें देश की एकता और अखंडता को खत्म करने की साजिश के तहत देशद्रोह की सजा मिलनी चाहिए क्योंकि ये देश के भीतर हिंसक दंगे भडक़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी अदालतों के जज जुबानी जमाखर्च को काफी मान लेते हैं, और अपने लिखित आदेशों को दीमक का लंच-डिनर बनते देखने में भी उन्हें कुछ बुरा नहीं लगता। ऐसे देश में ऐसे खतरे कब तक टलेंगे, यह अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है।
दिल्ली विधानसभा के चुनाव सामने खड़े हैं, और जाहिर है कि पिछले कुछ चुनावों से लगातार वहां जीतकर आ रही आम आदमी पार्टी को कई किस्म के सवालों के लिए तैयार रहनी चाहिए। इस पार्टी के पिछले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि अभी कथित शराब घोटाले में जमानत पर छूटे हुए हैं, और एक बार फिर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, उनका अपने सरकारी घर पर खर्च फिर खबरों में हैं। 2020 में मुख्यमंत्री के सरकारी निवास पर साज-सज्जा और दीगर कामों के लिए 7.9 करोड़ का अनुमान लगाया गया था, और 8.6 करोड़ में वह काम दिया गया था। लेकिन दो बरस बाद जब वह काम पूरा हुआ तो उसकी लागत 33.66 करोड़ रूपए हो चुकी थी। ये भाजपा के लगाए गए आरोपों के आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर सामने आए हैं, और इन्हें केजरीवाल के विरोधी पहले दिन से ही बादशाह के शीश महल पर खर्च करार दे रहे थे। अभी कल केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यह आरोप लगाया कि केजरीवाल ने सीएम हाऊस में सरकारी खर्च पर कई ऐसी बहुत महंगी चीजें लगवाईं जिनका उन्होंने तो कभी नाम भी नहीं सुना था। उन्होंने याद दिलाया कि जब केजरीवाल राजनीति में आए थे, तो उन्होंने कसम खाई थी कि सरकारी कार या बंगला नहीं लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल ने एक के बाद बंगले लिए, और बाद में 45 करोड़ रूपए से कई एकड़ पर शीशमहल बनवाया। अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में पानी की सप्लाई के लिए इंतजाम तो नहीं किया, लेकिन चार सदस्यों के अपने परिवार के लिए 15 करोड़ रूपए का पानी का संयंत्र लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपने बंगले पर डिजाइनर मार्बल पर 6 करोड़ रूपए, आधुनिक पर्दों पर 6 करोड़ रूपए, ऑटोमेटिक दरवाजों पर 70 लाख रूपए, कालीनों पर 50 लाख रूपए, और स्मार्टटीवी पर 64 लाख रूपए खर्च किए। केन्द्रीय गृहमंत्री शायद सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट से ही आंकड़े गिना रहे थे। इस रिपोर्ट में सीएजी ने बंगले पर किए गए खर्च के आधे से अधिक हिस्सा कलात्मक, ऐशोआराम के सामान, सजावटी सामान गिनाए थे जिन्हें पीडब्ल्यूडी ने एक्स्ट्रा आइटम बताते हुए वह खर्च किया था।
हम यहां पर कोई समाचार नहीं बना रहे हैं जिसमें एक-एक जानकारी और एक-एक आंकड़े देना जरूरी हो। हम तो महज इस पूरे विवाद पर अपनी सोच सामने रख रहे हैं कि किस तरह गांधी टोपी और खादी को खाल की तरह ओढक़र अन्ना हजारे नाम का एक आदमी यूपीए सरकार को हटाने की नीयत से एक वक्त आमरण अनशन पर बैठ गया था, और उस वक्त इस भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में शामिल केजरीवाल और उनके साथी तरह-तरह की सादगी की बातें करते हुए मनमोहन सरकार को खत्म करने की मुहिम छेड़े हुए थे। उस वक्त केजरीवाल ऐसे ढीले कपड़े पहनकर जनता के सामने रहते थे कि एक वक्त के खाते-पीते इंसान के अब भूखे मरने के दिन आ गए हैं, और मानो ये कपड़े बता रहे हों कि यूपीए सरकार के राज में केजरीवाल खा भी नहीं पा रहे हैं। वहां से लेकर आम आदमी पार्टी नाम का राजनीतिक दल बनाना, चुनाव लडऩा और कई बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना केजरीवाल का राजनीति के आसमान पर सूरज की तरह दमकना था। लेकिन गांधीवादी सादगी और आमरण अनशन के बीच से नेता बना यह नौजवान कब ऐसे ऐशोआराम का हिमायती हो गया वह पता ही नहीं लगा। कहां तो वह सरकारी बंगला और गाड़ी नहीं लेने वाला था, और अब जब बंगलों का शौक सिर चढक़र बोलने लगा, तो अपनी पार्टी के नाम के ठीक खिलाफ जाकर केजरीवाल नाम के स्वघोषित आम आदमी ने अपने आप पर आधा अरब रूपया खर्च करके अपने आपको दिल्ली का सबसे खास आदमी साबित किया, जनता के पैसों से।
हो सकता है कि केन्द्र सरकार, और दूसरी राज्य सरकारों में भी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के खर्च इसी दर्जे के होते हों, लेकिन हमें ऐसे दूसरे नेता याद नहीं पड़ते जिन्होंने सत्ता पर आने के लिए केजरीवाल की टक्कर के सादगी के नारे उछाले रहे हों। हमें यह जरूर याद पड़ता है कि त्रिपुरा में सीपीएम के एक से अधिक मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो परले दर्जे की सादगी की जिंदगी जीते रहे, और एक अकेले मुख्यमंत्री अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ एक ही कमरे में रह लेते थे, अपने-अपने कपड़े धो लेते थे, और एक ही कार में बैठकर ऑफिस जाना-आना कर लेते थे। एक दूसरे मुख्यमंत्री की पत्नी केन्द्र सरकार के किसी दफ्तर में काम करती थी, और मुख्यमंत्री निवास से ऑटोरिक्शा में अपने दफ्तर आने-जाने का इंतजाम खुद करती थीं। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि इस देश ने कभी सादगी और ईमानदारी देखी नहीं है। और लोगों ने केजरीवाल पर भरोसा कर लिया था कि वे स्वघोषित गांधीवादी और खादी ओढ़े हुए, आमरण अनशन पर बैठे हुए अन्ना हजारे के सबसे करीबी साथी बने हुए महीनों तक मीडिया में छाए रहे थे, और आम आदमी के नाम पर पार्टी बनाने के बाद सादगी का नारा देकर वे सत्ता पर पहुंचे थे।
हमारा यह मानना है कि देश की किसी भी सरकार को अपने नेताओं और अफसरों के लिए, जजों, और दूसरे ओहदों पर बैठे लोगों के लिए बंगले बनवाना बंद कर देना चाहिए। कई-कई एकड़ पर दर्जनों या सैकड़ों करोड़ की लागत से बनने वाले ऐसे बंगलों का रख-रखाव भी दसियों लाख रूपए महीने बैठता है, फिर चाहे इसे किसी एक सरकारी मद में एक साथ न दिखाया जाता हो। यह विकराल खर्च उस जनता के खून-पसीने की कमाई से निकाला जाता है जिसका पेट भरने के लिए उसे हर महीने पांच किलो चावल देने की नौबत देश में बनी हुई है। सरकारों को हर ओहदे का एक भत्ता तय करना चाहिए, उतने में वे जैसा चाहे वैसा मकान लें, चाहे तो अपने ही घर में रहते हुए उतना मकान भत्ता ले लें, और एक सीमित रकम उन्हें रख-रखाव के लिए मिलनी चाहिए। हालांकि हमारा पूरा भरोसा है कि ऐसा कोई सुझाव जनहित याचिका की शक्ल में भी अगर किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, तो शायद ही कोई जज इसे जनहित के नजरिए से देख पाएंगे, क्योंकि अनुपातहीन ऐशोआराम पाने वाले लोगों में बड़े जज भी तो सबसे आगे हैं। हमें छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बनने का दौर याद है जब राज्य सरकार के रखे गए बजट से असंतुष्ट जजों ने सरकार से और भारी-भरकम मंजूरी करवाई थी, और सरकार ने न चाहते हुए भी वह मंजूरी दी थी।
भारतीय लोकतंत्र अभी तक एक राजतंत्र और सामंती व्यवस्था के मुताबिक चलता है। यहां सत्ता पर काबिज तमाम राजा प्रजा के खून-पसीने पर बंगलों को महल में बदलने पर उतारू रहते हैं, और जब तक सत्ता शाही सहूलियतों में सांस लेगी, वह गरीब रियाया की तकलीफों से अनजान बनी रहेगी। इस सिलसिले को तोडऩा चाहिए, आज अमित शाह ने केजरीवाल पर हमला बोला है, और इसी तथ्य और तर्क का विस्तार करते हुए किसी जनसंगठन को पूरे देश में जनता के पैसों पर चलने और पलने वाली सरकारों के खुद पर खर्च का सोशल ऑडिट करना चाहिए।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर का कत्ल राज्य के मीडिया को हिला गया है। मुकेश नौजवान और बहुत सक्रिय पत्रकार थे, वे एनडीटीवी से भी जुड़े हुए थे, और उनका अपना यूट्यूब चैनल भी खासा लोकप्रिय था। इसके अलावा बस्तर के कुछ दूसरे पत्रकारों की तरह वे पत्रकारिता से परे भी सक्रिय रहते थे, और एक वक्त सरकारी कर्मचारी के नक्सल अपहरण के बाद उसकी रिहाई में भी उनका योगदान था। उनका कत्ल एक ठेकेदार के अहाते में ठेकेदार के भाई के हाथों हुआ बताया जा रहा है, और आज कुछ घंटों बाद पुलिस इसका खुलासा करने जा रही है। इस बीच जो जानकारी सामने आई है वह बस्तर में पत्रकारिता को लेकर कई बुनियादी सवाल खड़े करती है जिन पर सोचना-विचारना चाहिए।
जिस ठेेकेदार से यह मामला जुड़ा हुआ है, वह ठेकेदार सौ-पचास करोड़ के सडक़ ठेके वाला है, और बस्तर में ऐसे कई बड़े ठेकेदार अपनी कल तक की आर्थिक क्षमता से एकदम आगे बढक़र अचानक बड़े-बड़े काम करने लगते हैं, और इनमें से कुछ के बारे में यह जानकारी आम रहती है कि उनके नाम से पुलिस के कौन से बड़े अफसर ठेके लेते हैं। बस्तर में नक्सल हिंसा और खतरे के चलते कोई निर्माण ठेका ले लेने के बाद भी उसे पूरा करना तब तक नहीं हो सकता, जब तक पुलिस की खास मेहरबानी और हिफाजत उसे हासिल न हो। एक वक्त तो ऐसा था कि बस्तर के एक बड़े आईजी के बंगले पर ही पड़ोसी राज्य से आए हुए बड़े ठेकेदार रहते थे, और वहीं पर सारे ठेके तय कर दिए जाते थे। ऐसे सरकारी और कारोबारी माहौल में जो पत्रकार काम करते हैं, वे एक तरफ तो नक्सल खतरा झेलते हैं, और दूसरी तरफ अपने मीडिया-दफ्तर के दबाव भी झेलते हैं कि वहां से विज्ञापन वसूल करके भेजे जाएं, या सीधे-सीधे उगाही की जाए। छोटी जगहों पर काम करने वाले किसी भी दर्जे के संवाददाता तकरीबन बिना तनख्वाह के ही काम करते हैं, उन्हें कोई विज्ञापन कमीशन मिल जाता है, या फिर उनका संस्थान यह मान लेता है कि एक परिचय पत्र या एक माइक्रोफोन-आईडी के बाद संवाददाता खुद सारा इंतजाम कर सकते हैं, और अपने मुख्यालय को भी इश्तहार या उगाही भेज सकते हैं। ऐसे खतरनाक कारोबारी इंतजाम के साथ-साथ नक्सल खतरे के बीच बस्तर के अधिकतर पत्रकार काम करते हैं, और धीरे-धीरे वहां पत्रकारिता का वातावरण कारोबारी दबाव तले दम तोडऩे लगता है। फिर भी बहुत विपरीत परिस्थितियों में कुछ अच्छे पत्रकार लगातार हथियारबंद संघर्ष वाले इलाकों में काम करते हैं, और उन्हीं की वजह से जमीनी हकीकत सामने आती है। अभी मुकेश चंद्राकर के गुजर जाने पर कुछ लोगों ने इस बात को उठाया भी है कि किस तरह राजधानियों से बस्तर पहुंचने वाले पत्रकार वहां के स्थानीय पत्रकारों का इस्तेमाल करके अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, और स्थानीय पत्रकार हर तरह के दबाव, और खतरे झेलते हुए भी एक अच्छे आदिवासी मेजबान की तरह बाहरी प्रवासी पत्रकारों का साथ देने के लिए अपनी कई-कई दिन झोंक देते हैं।
हमने यह तमाम बातें नक्सल प्रभावित इलाकों में जर्नलिज्म का माहौल बताने के लिए लिखी हैं, और अब इनमें यूट्यूब जैसे प्लेटफार्म की वजह से शुरू हुई एक स्वतंत्र पत्रकारिता और जुड़ गई है, जिसमें मुकेश चंद्राकर और ऐसे कुछ नौजवानों ने खासा नाम कमाया है। लेकिन लगातार संघर्ष के इलाके में भारी भ्रष्टाचार के बीच काम करते हुए पत्रकार कई दूसरे तरह के प्रभावों से भी प्रभावित होते हैं। ऐसे में कब नक्सली, कब कारोबारी, कब पुलिस, कब नेता, और कब मीडिया का मैनेजमेंट उनका इस्तेमाल करते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। फिर किसी भी ऐसे पेशे में जहां पर नियमित आय की कोई गारंटी नहीं रहती है, लोगों को अपनी जिंदगी चलाने के लिए कई किस्म के जायज और नाजायज इंतजाम करने पड़ते हैं, और ऐसे में बस्तर के कई पत्रकार बड़े ठेकेदार भी बन जाते हैं, या ठेकेदारों के आपसी मुकाबलों में मोहरे बन जाते हैं। जब कभी बस्तर में रिपोर्टर किसी भी तरह फंसते हैं, या ठेकेदार, नेता, और अफसर अकेले या मिलकर उन्हें फंसा देते हैं, तो उनके संस्थान उनसे सबसे पहले हाथ धो लेते हैं, वे यह मानने से भी इंकार कर देते हैं कि ये संवाददाता कभी उनके लिए काम करते थे, या कर रहे हैं।
मुकेश चंद्राकर का कत्ल जिस बड़े ताकतवर और खाकी-मेहरबानी से लैस ठेकेदार के परिवार का किया गया बताया जा रहा है, उसके खिलाफ हाल ही में एक टीवी चैनल पर एक रिपोर्ट आई थी, और सौ-पचास करोड़ के इस ठेके की गड़बड़ी पर सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। इस रिपोर्ट में मुकेश चंद्राकर का भी योगदान बताया जा रहा है, और पारिवारिक संबंधों के बावजूद ऐसी रिपोर्ट पर ठेकेदार की निराशा थी, और वही कत्ल तक पहुंची दिख रही है। अब अगर इतने बड़े-बड़े ठेकों में गड़बड़ी की रिपोर्ट पर रिपोर्टर का कत्ल होने लगे, तो बड़े भ्रष्टाचार को भला कौन उजागर कर सकेंगे? और बस्तर जैसे इलाके में तो बड़े ठेकेदारों का ऐसा भ्रष्ट कारोबार आम है, और इसमें नेताओं और अफसरों की मेहरबानी और भागीदारी भी आम है। एक पत्रकार की हत्या को लेकर राज्य में लोकतंत्र के सभी पहलू विचलित हैं, और सरकार के पास भी अपने-आपको साफ साबित करने का एक मौका है क्योंकि हत्यारोपी परिवार कांग्रेस का करीबी, और पदाधिकारी बताया जा रहा है। बस्तर के पत्रकारों पर खतरा आज के इन कातिलों को सजा से खत्म नहीं होगा, और यह प्रकाशन और प्रसारण कारोबार की बाजारू रणनीतियों और तौर-तरीकों की वजह से पैदा चुनौती और खतरा भी है। मीडिया के लोगों को इस व्यापक मुद्दे पर सोचना-विचारना चाहिए, और सरकार को भी देखना चाहिए कि नक्सल इलाकों में उसके अफसर संविधानेतर सत्ता की तरह काम तो नहीं कर रहे हंै। इसके अलावा राजनीतिक दलों को भी कारोबारियों से कम से कम सार्वजनिक रूप से तो एक दूरी बनाकर रखना चाहिए। मुकेश चंद्राकर अच्छी टीवी रिपोर्टिंग करने वाले नौजवान थे, और उनके इस कत्ल के बाद इसे महज एक जुर्म की तरह जांच-परखकर और मामले को अदालत से फैसले तक पहुंचाने से परे भी सभी पहलुओं को सोचना चाहिए कि स्थितियों को कैसे सुधारा जा सकता है, और एक अच्छी पत्रकारिता को बस्तर में मौका कैसे दिया जा सकता है।
इन दिनों पूरे हिन्दुस्तान में जिस बड़े पैमाने पर साइबर-ठगी और जालसाजी चल रही है, और जिस तरह से गांव-गांव तक घुसकर कहीं चिटफंड, कहीं फाइनेंस कंपनी, कहीं क्रिप्टोकरेंसी, कहीं चेन मार्केटिंग का जाल बिछाया जा रहा है, वह भयानक है। अब ऐसा लगता है कि डकैती और लूट करने की किसी को जरूरत नहीं रह गई है, और बिना हथियार, बिना खून बहाए लोग करोड़पति और अरबपति हो रहे हैं। नमूने के लिए हम छत्तीसगढ़ की घटनाओं को लेते हैं जो कि बरसों से अखबारों में सुर्खियां बनी हुई हैं, और इनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि देश के दूसरे प्रदेशों में न हो रही हों। गांव-गांव तक जालसाजों के जाल फैल गए हैं, और सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी फर्जी फाइनेंस योजनाओं की मार्केटिंग में जुट गए हैं क्योंकि उसमें कमाई अधिक है। राज्य सरकार के बहुत से दूसरे कर्मचारी, और कई अधिकारी अपने परिवार के दूसरे लोगों के नाम से कुछ नामी-गिरामी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के सामानों की मार्केटिंग का नेटवर्क बढ़ाने में लगे हैं, और सरकार के पास पूरी जानकारी होने के बावजूद ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नेटवर्क मार्केटिंग तो सरकारी कुर्सी के असर का इस्तेमाल करके कमाई का एक जाल फैलाने का काम है, लेकिन बहुत तरह के ऐसे चिटफंड और फर्जी योजनाओं की खबरें लगातार आती हैं जिनमें एक-एक में हजारों लोग जिंदगी भर की कमाई डूबा चुके हैं, और कर्ज लेकर भी शेयर बाजार या क्रिप्टोकरेंसी के झांसे में पैसे लगा रहे हैं। ऐसी फर्जी योजनाओं में पैसा लगाने के लिए लोग ऑनलाईन कर्ज देने वाले देसी-विदेशी साहूकारों से पैसे ले रहे हैं, और वहां पर अलग लुट रहे हैं। आज इस तरह की साजिश का चमकता हुआ रंगीन बुलबुला जब फूटता है, तो इनमें पैसे फंसा चुके लोगों की आंखों में मानो बुलबुले के साबुन के छींटों से आंसू निकलने लगते हैं। उनका पैसा पंख लगाकर कई बैंक खातों से उड़ते हुए जाने कहां पहुंच चुका रहता है।
चूंकि राज्यों में केन्द्र सरकार की जांच और निगरानी एजेंसियों से कई गुना अधिक बड़ी मशीनरी अपनी खुद की है, इसलिए अगर राज्य सरकारें जागरूक रहें, तो वे समय रहते जालसाजी की ऐसी योजनाओं, उनकी कंपनियों, और उनके एजेंटों को पकड़ सकती हैं। हमने पहले भी इस बात का सुझाव दिया था कि राज्य सरकार को एक आर्थिक अपराध निगरानी ब्यूरो बनाना चाहिए। आज सरकार के पास आर्थिक अपराधों की जांच के लिए तो ब्यूरो है, सरकारी विभागों के भीतर भ्रष्टाचार पकडऩे के लिए भी छापामार दस्ते हैं, राज्य सरकार का अपना खुफिया विभाग भी है जो कि मोटेतौर पर राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर नजर रखता है, और इससे परे नक्सल इलाकों में खुफिया निगरानी के लिए सरकारी मशीनरी है। लेकिन सरकारी कामकाज से परे खुले बाजार में अगर फाइनेंस कंपनियां, चिटफंड कंपनियां, वॉट्सऐप जैसे मैसेंजरों पर पूंजीनिवेश के लिए फैलाए गए जाल काम कर रहे हैं, तो सरकार के पास इन पर खुफिया निगरानी रखने के लिए और समय रहते इनको दबोचने के लिए आज कोई ढांचा नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है। इनमें सरकार का पैसा तो सीधे-सीधे नहीं डूब रहा है, लेकिन राज्य की जनता का जितना भी पैसा धोखाधड़ी और जालसाजी में डूब जाता है, वह पैसा तो राज्य की अर्थव्यवस्था से बाहर चले जाता है, और पुलिस रिपोर्ट होने के बाद इन पर कार्रवाई करने का भारी-भरकम काम राज्य सरकार पर ही आता है। इसलिए राज्य सरकार को अपने नागरिकों को बचाने के लिए, और अपने खुद पर भविष्य में आने वाले विकराल बोझ को टालने के लिए एक आर्थिक अपराध निगरानी ब्यूरो बनाना चाहिए।
हमारा मानना है कि जितने भी किस्म की आर्थिक धोखाधड़ी की योजनाएं बाजार में फैलाई जाती हैं, वे किसी अंधेरी गली में बिकने वाले नशे की तरह नहीं रहतीं। इन योजनाओं को लोगों के बीच फैलाना पड़ता है, तभी जाकर लोग इसके झांसे में आते हैं। इस धोखाधड़ी को फुटपाथ पर किसी ताबीज बेचने वाले की तरह सपने दिखाकर ही कामयाब किया जा सकता है, और इसी वजह से यह एक संभावना बनती है कि अगर सरकार का कोई निगरानीतंत्र जनता के बीच लगातार काम करता रहे, तो बाजार में ऐसी बिछाई गई योजनाओं के बारे में समय रहते खबर लग जाएगी, और अधिक लोग डूबने से बच जाएंगे। आज तो हालत यह हो रही है कि धोखा खाए हुए लोगों में से कुछ लोग खुदकुशी कर चुके हैं, कई लोग जिंदगी भर की कमाई गंवा चुके हैं, और कई लोग कर्ज ले-लेकर ऐसी धोखाधड़ी में पूंजीनिवेश कर चुके हैं।
देश-प्रदेश में जुर्म किसी भी तरह का हो, उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी पुलिस या किसी सरकारी एजेंसी की आती है, और उसका कुल जमा कानूनी बोझ अदालत तक भी पहुंचता है। इन दोनों चीजों पर जनता का पैसा खर्च होता है, और यह बात जाहिर है कि देश की अदालतों पर करोड़ों मुकदमों का बोझ लदा हुआ है, और पुलिस की गिनती बढ़ती चली जाने के बावजूद बड़े पैमाने पर हो रही ऐसी जालसाजी और ठगी के लिए पुलिस हमेशा कम ही साबित होगी। आज नई टेक्नॉलॉजी की वजह से पुलिस और दूसरी जांच या निगरानी एजेंसियों के लिए यह बात कुछ आसान हो गई है कि समय पर जालसाजों की शिनाख्त होने से उनके फोन निगरानी में रखे जा सकते हैं, और उनके बैंक खातों को खाली होने के पहले जब्त किया जा सकता है। इन दिनों लगातार यह लग रहा है कि ठगी और जालसाजी भारत में एक सबसे बड़ा कारोबार बन चुके हैं, और लोगों को इससे कोई झिझक भी नहीं दिखती। जब आसपास के लोग ही अपने परिचित, दोस्त, और रिश्तेदारों को झांसा देने में लग जाते हैं, तो फिर ठगी-जालसाजी से लोगों का बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
राज्य सरकारों को अपने बंधे-बंधाए दायरे से परे भी कुछ सोचने की जरूरत है। अंग्रेजी में कहा जाता है कि सोच के बक्से से बाहर निकलकर कुछ सोचना चाहिए। ऐसी आऊट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से ही कोई राज्य सरकार एक निगरानी तंत्र विकसित कर सकती है जो कि डूब जाने के पहले जनता को बचा सके। यह एजेंसी एक लाईफ बेल्ट की तरह रहेगी जो कि किसी मोटरबोट के मुसाफिरों के लिए जरूरी रहती है, और डूबने से बचाती है। अगर यह न रहे तो सरकार को डूब चुकी लाशों को निकालने में सैकड़ों गुना अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हमारी यह कड़ी सिफारिश है कि सरकार को एक नई एजेंसी बनाकर जनता के बीच आर्थिक ठगी और जालसाजी पर निगरानी रखने, और समय रहते उसे पकडक़र सरकार की दूसरी एजेंसियों को कार्रवाई के लिए दे देने का काम करना चाहिए। यह एजेंसी तरह-तरह की साइबर-क्षमता वाली भी होनी चाहिए, जो कि जनता तक पहुंचने वाले झांसों को ऑनलाईन भी पकड़ सके। देखते हैं कि किस प्रदेश की सरकार ऐसी पहल करती है, और यह भी हो सकता है कि देश के किसी प्रदेश में ऐसा किया भी गया हो।