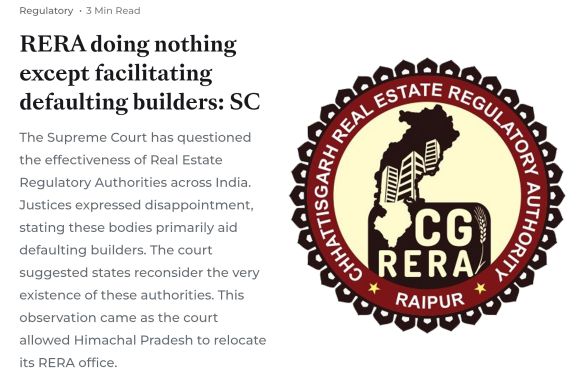संपादकीय
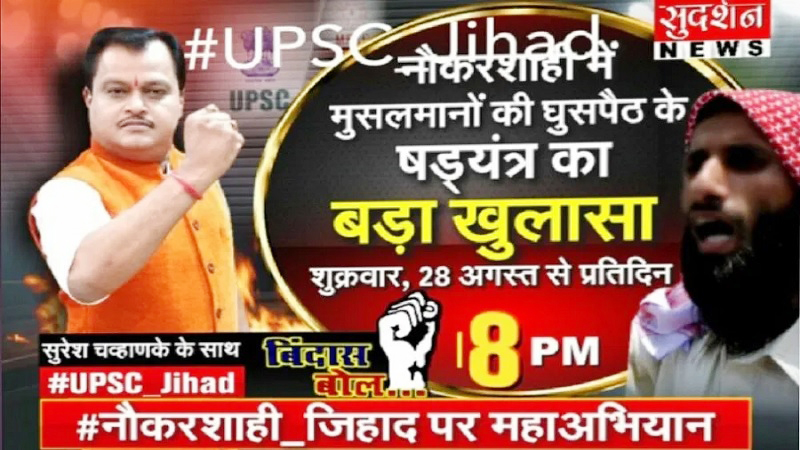
भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी.रमना ने देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जमकर कोसा है, और कहा है कि अदालतों में चल रहे मुद्दों पर गलत जानकारी देना और एक तय नीयत के साथ एजेंडा संचालित बहसें लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया अब भी कुछ हद तक जवाबदेह है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई जवाबदेही नहीं है, यह जो दिखाता है वह हवा-हवाई है। जस्टिस रमना रांची में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि मीडिया द्वारा प्रचारित पक्षपातपूर्ण विचार लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, और व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इससे न्याय प्रक्रिया पर भी उल्टा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि (इलेक्ट्रॉनिक) मीडिया अपनी जिम्मेदारियों के दायरे से आगे जाकर, और उनका उल्लंघन करके लोकतंत्र को पीछे ले जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया की हालत इससे भी बदततर है।
हमने इसी पन्ने पर पिछले बरसों में कई बार इस बात को लिखा है कि हिन्दुस्तान में मीडिया नाम का शब्द अब एक अटपटा लेबल बन गया है, और यहां के प्रिंट मीडिया को इससे बाहर निकलकर अपनी पुरानी पहचान, प्रेस को दुबारा कायम करना चाहिए। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चाल, चरित्र, चेहरा एक-दूसरे से इतना अलग है, दोनों की तकनीक अलग है, दोनों की जरूरतें और मकसद अलग हैं, और ऐसे में उन्हें एक दायरे में एक लेबलतले रखना कुछ ऐसा ही है जैसा कि एक हाथी और एक बकरी को मिलाकर उनका एक संघ बना दिया जाए। यह एक बेमेल काम होगा जिससे इन दोनों जानवरों में से किसी का भी मकसद पूरा नहीं होगा। किसी पेशे के दायरे में उस पेशे या कारोबारी संगठन में उस कारोबार से जुड़े हुए लोग इसलिए रहते हैं कि उनके हित एक सरीखे रहते हैं, उनकी जरूरतें मिलती-जुलती रहती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सारा ही तौर-तरीका अखबारनवीसी के पुराने और परंपरागत तौर-तरीकों से बिल्कुल ही उल्टा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कोई नीति-सिद्धांत हैं या नहीं, इसे वे ही बेहतर जानें, लेकिन हम प्रिंट मीडिया में पूरी जिंदगी गुजारने के बाद उसका यह निचोड़ सामने रख सकते हैं कि नीति-सिद्धांतों से परे प्रिंट मीडिया का कोई भविष्य नहीं है। आज भी कई अखबार घटिया निकलते होंगे, जो बिककर छपते होंगे, लेकिन ऐसे अखबार भी बने हुए हैं जो कि छपकर बिकते हैं। इसलिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक का यह बेमेल लेबल, मीडिया कम से कम प्रिंट को तो छोड़ देना चाहिए। प्रिंट के पास तो आजादी की लड़ाई के दिनों से अब तक चले आ रहा प्रेस नाम का एक खूबसूरत और इज्जतदार शब्द है, और उसे उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए।
यह बात हमारे सरीखे पेशेवर प्रिंट-पत्रकार ही नहीं कह रहे, इस देश के जागरूक नागरिकों का एक बड़ा तबका भी सोशल मीडिया पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस हद तक कोस रहा है कि यह हैरानी होती है कि देश में इतना कड़ा कानून रहते हुए भी टीवी चैनलों को लगातार नफरत और हिंसा फैलाने, लगातार साम्प्रदायिकता को बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है, और उन्हें इस काम के लिए बढ़ावा भी दिया जा रहा है। वैसे तो यह काम कुछ अखबारों को बढ़ावा देकर भी हो रहा है, लेकिन फिर भी अखबारों के एक हिस्से में अब तक एक दर्जे की सामाजिक जवाबदेही बाकी है, जो कि टीवी समाचार चैनलों पर कब की खत्म हो चुकी है।
देश के मुख्य न्यायाधीश अपनी अदालत के बाहर एक लॉ यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में तो यह बात बोल रहे हैं, लेकिन जब अनगिनत मामलों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फैलाई नफरत सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुकी है, तो वहां पर न तो मुख्य न्यायाधीश, और न ही दूसरे जज ऐसे नफरतजीवी, हिंसक, और देश को तबाह कर रहे टीवी चैनलों के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। जब ऐसे चैनलों के मालिक और संपादक बड़े-बड़े हमलावर हथियार लेकर कैमरों के सामने खड़े होते हैं, और देश से एक मजहब को, उसे मानने वाले लोगों को खत्म करने के फतवे देते हैं, तो ऐसे मामलों पर भी सुप्रीम कोर्ट का बर्दाश्त देखने लायक है। देश का ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, बल्कि देश के हाईकोर्ट भी जब चाहें तब व्यापक जनहित के मामलों को बिना किसी पिटीशन के भी खुद मामला बना सकते हैं, और सुनवाई शुरू कर सकते हैं। ऐसे में बेहतर तो यह होता कि मुख्य न्यायाधीश एक व्याख्यान में ऐसी मसीहाई बातें करने के बजाय जज की कुर्सी पर बैठकर अपनी तनख्वाह को जायज साबित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जुर्म के कुछ नमूनों को लेकर एक कमेटी बनाते, और वह कमेटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार से परे अपनी रिपोर्ट देती जिसमें सरकारी रूख का भी विश्लेषण रहता। आज सरकार के ऊपर मानो कुछ भी नहीं रह गया है, संसद में सरकारी बाहुबल के सामने विपक्ष को अनसुना कर देना एक परंपरा बन गई है। देश में सबसे महंगा संसद भवन बन रहा है, और बिना बहस कानून बनाना उसके भीतर इस बाहुबल के लिए सबसे सस्ता काम रहेगा। ऐसे में अदालत को ही यह देखना होगा कि सरकारी अनदेखी किस कीमत पर चल रही है, उससे लोकतंत्र का कितना नुकसान हो रहा है।
मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक प्रक्रिया को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हरकतों की चर्चा की है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नुकसान इस देश में न्याय प्रक्रिया से परे आम जनता को भी झेलना पड़ रहा है, और इस देश का परंपरागत ताना-बाना छिन्न-भिन्न हो चला है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को न्याय प्रक्रिया के सामने टीवी चैनलों की खड़ी की हुई दिक्कत को ही नहीं देखना चाहिए बल्कि यह भी देखना चाहिए कि लोकतंत्र को जो व्यापक नुकसान इस संगठित बड़े कारोबार द्वारा सोच-समझकर, और सरकारी अनदेखी या बढ़ावे से किया जा रहा है, उसे कैसे रोका जाए? समाज के भीतर एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत के सैलाब में डुबाकर, हथियार थमाकर जिस तरह लड़ाया जा रहा है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट को ही देखना होगा क्योंकि सरकार की दिलचस्पी इसमें नहीं दिख रही है।
जस्टिस एन.वी. रमना की कही बातें अगर उनके आखिरी कुछ हफ्तों में कोई शक्ल नहीं लेती हैं, तो ये किसी काम की नहीं रहेंगी। आज उन्हें कोई नहीं रोक सकता अगर वे अपने इन आखिरी हफ्तों में हिन्दुस्तान में टीवी चैनलों की नफरत और हिंसा और उसकी सरकारी अनदेखी की जांच करें। उन्हें तुरंत प्रिंट-मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और रिटायर्ड जजों में से लोगों को छांटकर ऐसी कमेटी बनानी चाहिए। इसकी रिपोर्ट तो जस्टिस रमना के रिटायर होने के बाद ही सामने आ पाएगी, लेकिन ऐसा काम उनके नाम के साथ जरूर दर्ज होगा।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)