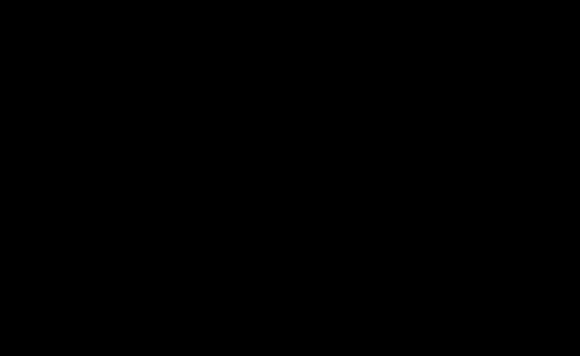विचार/लेख
-दिलनवाज पाशा
बांग्लादेश ने चार महीने पहले हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से ऐसे कई कदम उठाए हैं, जिनसे उसके पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर होने के संकेत मिलते हैं।
बुधवार को बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने के लिए जरूरी सुरक्षा जांच के नियम को भी हटा दिया।
बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान किया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तानी लोगों और पाकिस्तान मूल के लोगों को वीजा दिया जाए। वहीं, पाकिस्तान ने सितंबर में बांग्लादेश के नागरिकों के लिए वीजा फीस माफ कर दी थी और वीजा प्रक्रिया को आसान कर दिया था।
साल 2019 में शेख हसीना सरकार ने बांग्लादेश का वीज़ा लेने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों के लिए बांग्लादेश की सिक्योरिटी सर्विस डिवीजन से सुरक्षा मंज़ूरी लेना अनिवार्य किया था।
अब इस नियम को भी हटा दिया गया है।
ये सत्ता परिवर्तन के बाद से बांग्लादेश के ऐसे कई क़दमों में से एक है, जिनसे ये संकेत मिलते हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पाकिस्तान के कऱीब दिखने की कोशिश कर रही है।
बांग्लादेश ने बदला रुख़
बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ गोला बारूद की खऱीद के लिए रक्षा सौदे भी किए हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच पांच दशक बाद समुद्री रास्ते से कारोबार भी शुरू हुआ है।
पहली बार, पाकिस्तान का मालवाहक जहाज हाल ही में बांग्लादेश के चिट्टागांव बंदरगाह पहुंचा है।
यही नहीं, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 25 हजार टन चीनी खरीदने के लिए भी सौदा किया है। बांग्लादेश अब तक भारत से चीनी आयात करता रहा था।
शेख हसीना सरकार के जाने के कुछ वक्त बाद ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर गोला-बारूद खऱीदने के लिए सौदा किया।
1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश के अस्तित्व में आमने के बाद से, दोनों देशों के बीच रहे ऐतिहासिक तनाव को देखते हुए इस घटनाक्रम को अहम पड़ाव माना जा रहा है।
बांग्लादेश में शेख़ हसीना के शासन के दौरान भारत की तरफ झुकाव रहा और शेख हसीना सरकार ने भारत के साथ रिश्ते मज़बूत करने पर जोर दिया।
भारत से जुड़े बांग्लादेश के हित
बांग्लादेश के साथ करीब चार हजार किलोमीटर की सीमा साझा करने वाला भारत भी बांग्लादेश से रिश्ते मजबूत करने पर जोर देता रहा है।
और इसके लिए भारत ने बांग्लादेश में भारी निवेश भी किया। भारत बांग्लादेश को एक अहम रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखता रहा है।
यही वजह है कि पाकिस्तान की एक लंबे दौर तक बांग्लादेश से दूरी बनी रही।
लेकिन, अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में चल रही अंतरिम सरकार बांग्लादेश के भू-राजनैतिक दृष्टिकोण को बदल रही है। और भारत पर निर्भरता कम करने के प्रयास कर रही है।
बांग्लादेश भी पाकिस्तान के कऱीब जाकर शायद ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह अब दक्षिण एशिया की राजनीति को भारत के नज़रिए से नहीं देखेगा।
‘भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं’
लेकिन विश्लेषकों को लगता है कि बांग्लादेश के लिए लंबे समय तक पाकिस्तान के कऱीब रहना आसान नहीं होगा।
अंतरराष्ट्रीय मामलों की जानकार स्मृति एस पटनायक कहती हैं, ‘बांग्लादेश भले पाकिस्तान के करीब जाता दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होना आसान नहीं है। बांग्लादेश के आर्थिक हित भारत के साथ जुड़े हैं।’
हालांकि वो ये भी कहती हैं, ‘बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही स्वतंत्र देश हैं और कारोबारी रिश्ते बना सकते हैं, भारत को इसे लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए।’
‘बाजार के अपने नियम हैं और बांग्लादेश के लिए भारत की जगह पाकिस्तान के साथ कारोबार को बढ़ावा देना उसके आर्थिक हित में नहीं होगा।’
हालांकि, विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि हाल के महीनों के जो घटनाक्रम हुए हैं, उनसे बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब जाता हुआ दिख रहा है।
‘बांग्लादेश अस्थिरता के दौर में’
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार और जवाहर लाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर संजय भारद्वाज कहते हैं कि बांग्लादेश इस समय अस्थिरता के दौर में हैं।
उनका कहना है कि इस्लामी विचारधारा के करीब जाना वहां की अंतरिम सरकार की राजनीतिक मजबूरी भी है।
संजय भारद्वाज कहते हैं, ‘जब-जब बांग्लादेश में सरकार के सामने संकट आया है या फिर संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, तब-तब तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और इस्लामी विचारधारा के करीब दिखने की कोशिश करता रहा है।’
‘1975 में शेख़ मुज़ीबुर्रहमान की हत्या के बाद आए अगले शासन ने बांग्लादेश का इस्लामीकरण करने की कोशिश की।’
‘इसके बाद बांग्लादेश में सैन्य शासन के दौरान भी इस्लामीकरण की कोशिश हुई, ताकि बांंग्लादेश का एक वर्ग जो इस्लाम और पाकिस्तान के विचार में विश्वास करता है, उसका साथ मिल जाए।’
‘अब भी ऐसा लग रहा है कि वहां कि अंतरिम सरकार वैधता हासिल करने के लिए इस्लामी विचारधारा से प्रभावित वर्ग को अपने साथ लाने के प्रयास कर रही है।’
जब बांग्लादेश बना था
बांग्लादेश 1971 में हिंसक संघर्ष के बाद पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना था और भारत में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेशी राष्ट्रवादियों की सैन्य और राजनीतिक मदद की थी।
प्रोफ़ेसर संजय भारद्वाज कहते हैं, ‘बांग्लादेश में जो बंगाली-सांस्कृतिक विचार है वह धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है। बांग्लादेश की बंगाली संस्कृति धर्म निरपेक्ष और समावेशी है।’
‘यानी लोकतांत्रिक भारत के अधिक कऱीब है। ऐसे में नए शासन के लिए इस्लामी विचारधारा और पाकिस्तान के लिए कऱीब दिखना राजनीतिक मजबूरी अधिक नजऱ आती है।’
विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ संबंध मज़बूत करते दिखना बांग्लादेश की भारत को संदेश देने की कोशिश भी है।
स्मृति पटनायक कहती हैं, ‘शेख हसीना के दौर में दोनों देशों के बीच नजदीकी रिश्ते नहीं थे। लेकिन उस दौर में भी बांग्लादेश के राजनयिक पाकिस्तान में थे। हसीना के कार्यकाल के मुकाबले जरूर पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं।’
उन्होंने बताया, ‘भले ही आर्थिक रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश के नजदीक आने में चुनौतियां हों लेकिन वैचारिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आ सकते हैं।’
क्या भारत के लिए चिंता की बात?
बांग्लादेश में इस्लामी विचारधारा का मजबूत होना भारत के लिए चिंता का कारण हो सकता है।
हालांकि, ये सवाल भी है कि क्या 1971 युद्ध के बाद पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश अब फिर से पाकिस्तान के इतना कऱीब आ सकता है कि भारत के लिए ख़तरा पैदा हो जाए?
विश्लेषक मानते हैं कि ऐसा होना आसान नहीं होगा।
प्रोफेसर संजय भारद्वाज कहते हैं, ‘1947 में बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन वह पाकिस्तान के साथ नहीं रह पाया। उसके सांस्कृतिक और भोगौलिक कारण थे। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि बांग्लादेश और पाकिस्तान बहुत अधिक कऱीब आ पाएंगे।’
‘बांग्लादेश की बड़ी आबादी बंगाली राष्ट्रवाद, धर्म-निरपेक्षता और समावेशी व्यवस्था में यकीन करती है और यही विचारधारा बांग्लादेश को भारत के अधिक करीब ले आती है।’
लेकिन, बांग्लादेश का पाकिस्तान के कऱीब आना भारत के लिए कई स्तर पर चुनौती जरूर पैदा करेगा।
खासकर पूर्वोत्तर के साथ बांग्लादेश की लंबी सीमा को देखते हुए।
स्मृति पटनायक कहती हैं, ‘भारत की मुख्य चिंता सुरक्षा और पूर्वोत्तर में स्थिरता को लेकर होगी। भारत नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश के साथ उसका सीमा क्षेत्र अस्थिर हो और वहां सीमा के उस पार से सुरक्षा ख़तरा पैदा हो। अगर बांग्लादेश पूर्वोत्तर के मिलिटेंट तत्वों को शरण देता है तो इससे भारत के लिए ज़रूर चिंता पैदा होगी।’
वहीं बांग्लादेश में इस्लामी विचारधारा और कट्टरवादी तत्वों का मजबूत होना भी भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं पैदा कर सकता है।
स्मृति कहती हैं, ‘बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष ताकतें भी हैं, आगे ये देखना होगा कि वहां इस्लामवादी विचारधारा अधिक मजबूत होती है या धर्म निरपेक्ष।’
प्रोफेसर संजय भारद्वाज कहते हैं, ‘किसी भी पड़ोसी देश में राजनीतिक अस्थिरता, कट्टरवाद का उदय चिंताजनक होता है। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक वर्ग पर ख़तरा बढ़ जाता है।’
-डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
सोशियल मीडिया में जिस तरह से आजकल शार्टकट मैसेज को प्राथमिकता दी जाने लगी है वह किसी मानसिक प्रताडऩा से कम कर नहीं आंकी जा सकती। कारण भी साफ है सोशियल मीडिया के संदेशों को डीकोड करने की अपनी समस्या सामने आने लगी है। यह कोई कपोल कल्पित परिकल्पना नहीं अपितु अमेरिका के स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसंधान कर्ताओं के एक दो नहीं अपितु 8 शोध का परिणाम है। यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं या यों कहें कि सर्वेकर्ताओं को शोध परिणाम जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंक में प्रकाशित हुआ है। दरअसल आज के व्यक्ति को फुर्सत ही नहीं है अपनी बात दूसरे को सलीके से कहने की। जिस तरह से आज दैनिक जीवन में शार्टकट का सिलसिला चल निकला है ठीक उसी तरह से एक दूसरे को मैसेज भी शार्टकट में दिए जाने लगे हैं। कई बार तो हालात यह हो जाती है कि सामने वाला उसे डीकोड करने में बुरी तरह से झुंझलाने लगा है। हो यह रहा है कि हम लाख होशियार हो पर सोशियल मीडिया के माध्यम से कम्यूनिकेशन का जो तरीका अपनाया जाने लगा है वह सामने वाले के लिए एक नया तनाव का कारण बनता जा रहा है।
बानगी के रुप में देखे तो आने वाले नए साल को लेकर एक मैसेज ड्ब्लूटीएफ इन दिनों बहुत चल रहा है। अब इस मैसेज को डीकोड करने में दो तरह की परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। मैसेजकर्ताओं द्वारा ड्ब्लूटीएफ का उपयोग मानव इतिहास के सबसे डऱावने सालों में से एक 2020 से जोडक़र किया जा रहा है। सीधे सीधे रुप से बात करें तो यह मैसेज आने वाले साल की शुरुआत वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राईडे यानी कि ड्ब्लूटीएफ से कर रहे हैं और लोगों को कोरोना त्रासदी की और ध्यान दिलाते हुए कि 2020 में भी साल की शुरुआत इसी तरह से हुई थी ऐसे में यह संदेश दिया जा रहा है कि आने वाला साल 2020 जितनी भले ही नहीं हो पर संकटपूर्ण होगा। यह केवल कपोल कल्पना हो सकती है पर इसका धडल्ले से उपयोग हो रहा है। दूसरी और इस ड्ब्लूटीएफ का ही दूसरा मतलब है कि व्हाट द फक यानी कि क्या मजाक है। यानी इस एक शार्टकट मैसेज के माध्यम से सोशियल मीडिया पर ड्ब्लूटीएफ के माध्यम से डऱावना भी बताया जा रहा है तो दूसरी और ड्ब्लूटीएफ को क्या मजाक है के रुप में पहले अर्थ या पहली व्याख्या को नकारा भी जा रहा है। यह तो एक मिसाल मात्र है।
मजे की बात यह है कि सोषियल मीडिया पर मैसेज के माध्यम से ही बहुत बड़ी संख्या में लागों की शुरुआत होने लगी है। वह जीएम यानी कि गुड़ मोर्निंग से शुरु होते हुए जन्म दिन की शुभकामनाएं तो एचबीडी, डीएलवाई मतलब अपने आप करों, फोमो यानी की कुछ छूट जाने का डऱ, ओटी मतलब ऑपरेशन थियेटर ना होकर विषय से परे या यों कहे कि आउट ऑफ टोपिक, एनपी लिखकर आप कोई प्रोबलम नहीं का संदेश दे देते हो। किसी का फोन आया और आप बात नहीं कर पाये तो टीटीवाईएल मैसेज कर देते हो जिसे डीकोड करने पर ही पता चलता है कि टाक टू यू लेटर यानी बाद में बात करता हूं। कोई जानकारी आपसे चाहता है तो आप शार्टकट के सहारे आईडीके लिख कर इतिश्री कर लेते हैं अब समझने वाला अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर डीकोड करेगा कि आप कहना चाहते हैं कि आई डोन्ट नो। यह तो कुछ उदाहरण मात्र है जिनका उपयोग अत्यधिकता में होने लगा है। यह तो टैक्स्ट मैसेज की बात है इमोजी मैसेज की दुनिया तो इससे भी अलग है। मजे की बात यह है कि इनका प्रयोग बहुतायत में होने लगा है।
दरअसल कम्यूनिकेशन भी एक कला है। एक समय था जब बच्चों की कम्यूनिकेशन स्कील विकसित की जाती थी। अब सोशियल मीडिया के इस जमाने में कम्यूनिकेशन स्कील तो दूर की बात शार्टकट के आधार पर ही काम चलाया जा रहा है। मजे की बात यह है कि सामने वाले से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे सबकुछ मालूम है। जबकि मैसेज प्राप्त करने वाले इसी उधेड़बुन में उलझ जाता है कि इसका मतलब क्या है? दूसरा से भी संकोच के कारण पूछ नहीं पाता। मनोचिकित्सक डॉ. नावा सिलटॉन का मानना है कि इस तरह के मैसेज सामने वाले में झुंझलाहट पैदा करने से अधिक कुछ नहीं कर पाता। देखा जाए तो बिना मांगे मानसिक तनाव प्राप्त करना है। देखा जाए तो कोई भी मैसेज करने की सार्थकता इस में होनी चाहिए कि सामने वाला एक नजर में समझ जाएं कि मैसेज में कहना क्या चाहा गया है। मजे की बात यह है कि आज की पीढ़ी पर भी इसका विपरीत परिणाम सामने आने लगा है। शार्टकट से काम चलाने के चक्कर में मैसेज के साथ जो भावनात्मकता होती है वह कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती और केवल डीकोड करने में ही समय जाया हो जाता है।
शेख़ हसीना के सत्ता से बेदख़ल होने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान में करीबी बढ़ाने की वकालत कई स्तरों पर हो रही है।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भी ऐसे कई संकेत दिए हैं। मसलन पिछले महीने पाकिस्तान का मालवाहक पोत कराची से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुँचा था। बांग्लादेश बनने के बाद दोनों देशों के बीच यह पहला समुद्री संपर्क था।
तीन दिसंबर को पाकिस्तानी मीडिया में ख़बर छपी कि दशकों बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी आयात की है, जो अगले महीने कराची बंदरगाह से बांग्लादेश चटगाँव बंदरगाह पर पहुँचेगी।
पाकिस्तानी अख़बार द न्यूज ने लिखा है, ‘इससे पहले बांग्लादेश भारत से चीनी आयात करता था।’
बांग्ला अखबार ढाका पोस्ट की खबर को शेयर करते हुए बांग्लादेश के सुमोन कैस नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है, ‘चीनी का आयात पहले भारत से होता था। लेकिन अब उसने यह मौका खो दिया है। 2014 के बाद बांग्लादेश के पशु बाजार से भी भारत बाहर हो गया है। मैं इस बात को लेकर भी आश्वस्त हूँ कि आने वाले वक्त में भारत का कॉटन भी बांग्लादेश नहीं आएगा।’
‘एक दिन ऐसा भी आएगा, जब बांग्लादेश और भारत का द्विपक्षीय व्यापार 16 अरब डॉलर से कम होकर एक या दो अरब डॉलर तक सीमित हो जाएगा। दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन भारत? हम खरीददार हैं और हमारे पास पैसे हैं, ऐसे में हमें जहाँ से खरीदने का मन होगा, वहाँ से खरीदेंगे। थर्ड क्लास की नीति दादागिरी अब नहीं चलेगी।’
पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम का ढाका में कार्यक्रम था। इसमें हजारों लोगों की भीड़ जुटी थी। 29 नवंबर को आतिफ असलम का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें दिख रहा है कि वह ढाका की सडक़ पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं।
‘पाकिस्तान का परमाणु बम आपके लिए’
सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि भीड़ को एक व्यक्ति मंच से संबोधित कर रहा है। इनमें से दो लोगों के हाथ में पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्रध्वज हैं।
वह व्यक्ति कह रहा है, ‘आज हम अपने बंगाली भाइयों को जवाब देते हैं। उन्हें बताते हैं कि भाई यह पाकिस्तान तुम्हारा है।’
‘इस पाकिस्तान का जो एटम बम है न, वो भी तुम्हारा है। आए ज़ुर्रत करे कोई, बांग्लादेश की तरफ आँख उठाकर देखने की, उसकी आँखें निकाल देंगे। अल्ला के फजल से हम बांग्लादेश पर हाथ उठाने वाले के बाज़ू तोड़ देंगे। मैं उस मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता।’
भीड़ इस संबोधन पर उत्साह से लबरेज होकर ताली बजाती है और फिर बांग्लादेश जि़ंदाबाद के नारे लगते हैं। इसी तरह बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्ज़मां का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह पाकिस्तान के साथ परमाणु समझौते की वकालत कर रहे हैं। यह वीडियो अगस्त में शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद सितंबर महीने का है।
रिटायर्ड आर्म्ड फ़ोर्सेज ऑफिसर्स वेलफेयर्स असोसिएशन के एक सेमिनार को संबोधित करते हुए प्रोफेसर शाहिदुज्जमां ने कहा था, ‘हमें पाकिस्तान के साथ परमाणु करार करना चाहिए। बिना गठजोड़ और तकनीक के भारत का सामना नहीं किया जा सकता है। भारत को लगता है कि बांग्लादेश पूर्वोतर का उसका कोई आठवां राज्य है। भारत की इस अवधारणा को परमाणु ताकत से ही तोड़ा जा सकता है।’
प्रोफेसर शाहिदुज्जमां ने कहा था, ‘बांग्लादेश में ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यह अवास्तविक है और साथ ही बहुत महंगा है। परमाणु ताक़त केवल इसे बनाने से ही हासिल नहीं होती है बल्कि हम पाकिस्तान से कऱार कर सकते हैं। बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार है। भारत नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छा रहे। हम पाकिस्तान की मदद से उत्तर बंगाल में मिसाइल तैनात कर सकते हैं।’
पाकिस्तान के लिए मौक़ा?
प्रोफ़ेसर शाहिदुज्ज़मां के इस बयान को पाकिस्तानी मीडिया में भी काफ़ी तवज्जो मिली थी। पाकिस्तान के प्रमुख अंग्रेजी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने प्रोफेसर शाहिदुज्ज़मां का हवाला देते हुए लिखा था कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच चीजें तेजी से बदल रही हैं।
प्रोफेसर शाहिदुज्ज़मां की यह बात पाकिस्तान में हाथोंहाथ ली गई। पाकिस्तानी पत्रकार कामरान युसूफ ने लिखा, ‘ढाका यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय संबंध के प्रोफेसर शाहिदुज्ज़मां ने भारत का सामना करने के लिए पाकिस्तान से परमाणु करार का प्रस्ताव रखा है।’
कामरान ने लिखा है, ‘जब वह प्रस्ताव रख रहे थे तो बांग्लादेश के लोगों ने तालियों की गडग़ड़ाहट के साथ स्वागत किया। यहाँ तक कि प्रोफेसर शाहिदुज्ज़मां ने पाकिस्तान की मध्यम दूरी की गौरी मिसाइल भारत से लगी सीमा पर तैनात करने की वकालत की।’
‘एक दिन बाद एक और प्रोफेसर ने शाहिदुज्ज़मां के आइडिया का समर्थन किया। मैंने प्रोफ़ेसर शाहिदुज्ज़मां के वीडियो के नीचे कॉमेंट को स्क्रॉल कर देखा तो बांग्लादेश के लोग भारी समर्थन दे रहे थे। एक भी कॉमेंट प्रोफ़ेसर शाहिदुज्ज़मां के आइडिया के खिलाफ नहीं था।’
कामरान युसूफ लिखते हैं, ‘सवाल ये नहीं है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच परमाणु करार संभव है या नहीं। अहम बात यह है कि बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान को लेकर बदल रहे हैं। बंगालियों के साथ पाकिस्तान ने नाइंसाफी की थी लेकिन वो धूल अब छँट चुकी है। प्रोफेसर शाहिदुज्ज़मां ने भी कहा कि 1971 में जो कुछ हुआ था, उससे पाकिस्तानी भी दुखी थे। कुछ महीने पहले तक बांग्लादेश में ऐसी सोच अकल्पनीय थी। शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते पाकिस्तान के साथ ऐसी गर्मजोशी असंभव थी।’
‘मोहम्मद युनूस से पीएम मोदी नहीं मिले’
अमेरिका में बांग्लादेश के राजदूत रहे एम हुमायूं कबीर का मानना है कि भारत के साथ संबंधों में जटिलता बढ़ती जा रही है।
हुमायूं कबीर ने बांग्लादेश के अख़बार प्रोथोमआलो से कहा, ‘भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध बहुआयामी रहे हैं। अभी भारत के साथ बांग्लादेश के आर्थिक संबंध एकतरफा है। हम भारत से बिजली, डीज़ल, चावल, प्याज और आलू आयात करते हैं। लेकिन बांग्लादेश से भारत बहुत कम चीज़ों का निर्यात होता है।’
‘भारत के साथ हमारा सांस्कृतिक संबंध भी रहा है। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पढ़ाई करने जाते थे। पिछले 15 सालों में बांग्लादेश के लोगों को भारत जाने के लिए वीज़ा आसानी से मिल जाता था लेकिन अगस्त के बाद से वीज़ा को लेकर सख्ती बढ़ गई है। भारत अगर संबंधों को ठीक करना चाहता है तो उसे वीज़ा देने की प्रक्रिया को उदार बनाना चाहिए।’
हुमायूं कबीर कहते हैं, ‘दोनों देशों के बीच तनाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भारत ने पाँच अगस्त के बाद बांग्लादेश की घरेलू राजनीति की हकीकत को स्वीकार नहीं किया। बांग्लादेश को भी सतर्क रहना चाहिए कि हालात कहीं बेकाबू ना हो जाएं। मुझे लगता है कि दोनों देशों में लोगों को उकसाने वाली गतिविधियां नहीं होनी चाहिए।’
हुमायूं कबीर ने कहा, ‘बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद डॉ़ मोहम्मद युनूस ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत के साथ संबंध बराबरी के आधार पर आगे बढ़ेगा। भारत के पत्रकारो से बात करते हुए भी मोहम्मद युनूस ने कहा था कि वह द्विपक्षीय संबंध बेहतर करना चाहते हैं।’
‘बांग्लादेश ने सितंबर में कोशिश की थी कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आमसभा के दौरान मोहम्मद युनूस की पीएम मोदी से मुलाकात हो लेकिन नहीं हो पाई। पाँच अगस्त के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए बहुत कोशिश नहीं की गई है।’
हुमायूं कबीर कहते हैं, ‘समस्या यह है कि बांग्लादेश में हुए राजनीतिक परिवर्तन को भारत स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इन्हें लगता था कि बांग्लादेश की केवल एक पार्टी से संबंध मजबूत रखना काफ़ी है। सभी को पता है कि 2014 में भारत की तत्कालीन विदेश सचिव सुजाता सिंह ने बांग्लादेश में चुनाव को कैसे प्रभावित किया था। इसे हमने 2018 और 2024 में भी देखा। भारत को यह समझना चाहिए कि बांग्लादेश के लोग क्या चाहते हैं।’
भारतीय मीडिया से नाराजग़ी
बांग्लादेश में भारतीय मीडिया को लेकर भी काफी ग़ुस्सा है। बांग्लादेश के अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार की पत्रकार नाजिबा बशर ने भारतीय मीडिया की कवरेज को लेकर ही अपने डिजिटल एडिटर एस्तानी अहमद से बात की।
अहमद ने इस बातचीत में कहा, ‘बांग्लादेश में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, उसे लेकर भारतीय मीडिया में किसी विदेशी साजिश की बात कही जाने लगी। भारतीय मीडिया आउटलेट्स में इसके पीछे अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की साजिश की बात कही जाने लगी।’
‘शेख हसीना के जाने के बाद भारतीय मीडिया में कहा जाने लगा कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान की तरह इस्लामिक देश बन जाएगा। अगर भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने की बात होती है तो भारतीय मीडिया को दिक्कत नहीं होती है लेकिन बांग्लादेश अगर मान लीजिए कि इस्लामिक देश बन भी जाता है तो इंडियन मीडिया को समस्या होने लगती है। ये मानकर चलते हैं कि इस्लामिक देश होने का मतलब हिंसक होना है।’
अहमद ने कहा, ‘बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से पहले यहाँ विदेशी पत्रकारों को वीजा के लिए कम से कम एक हफ्ता लग जाता था लेकिन अब एक रात में ही वीजा मिल जा रहा है। मोहम्मद युनूस चाहते हैं कि विदेशी पत्रकार आएं और सच्चाई देखें। सच्चाई वो नहीं है जो भारतीय मीडिया में दिखाया जा रहा है।’ (bbc.com/hindi)
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल को सोमवार को अकाल तख़्त की ओर से धार्मिक सजा सुनाई गई थी।
अकाल तख़्त सिख धर्म से जुड़ी सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है और उसे ये अधिकार है कि वो अपराधों के लिए किसी भी सिख को तलब करे और उसके खिलाफ धार्मिक सज़ा का एलान करे, जिसे ‘तन्खाह’ कहते हैं
सिख परम्पराओं के अनुसार, अगर कोई सिख, सिख धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ काम करता है या सिख समुदाय की भावनाओं के विपरीत काम करता है तो उसे अकाल तख़्त की ओर से धार्मिक सजा सुनाई जा सकती है।
दो दिसम्बर को सिख प्रतिनिधियों और सिखों के पांच प्रमुख धर्म स्थलों के मुखिया की अकाल तख़्त में मीटिंग हुई थी। और इसी मीटिंग में सुखबीर बादल समेत 2007 से 2017 के बीच उनके कैबिनेट में मंत्री रहे अधिकांश लोगों को धार्मिक सज़ा दी गई।
अकाल तख्त की ओर से 2015 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की कार्यकारिणी के सदस्यों और तख़्तों के कुछ पूर्व जत्थेदारों को भी समन किया गया था।
अकाली नेतृत्व को क्यों सजा दी गई?
साल 2007 से 2017 के बीच पंजाब में शिरोमणि अकाली दल-बीजेपी की गठबंधन सरकार थी।
दिवंगत अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल इस सरकार में मुख्यमंत्री थे जबकि सुखबीर बादल पार्टी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री थे।
अकाली दल के नेतृत्व पर सिख धर्म के सिद्धातों और सिख समुदाय की भावनाओं के विपरीत काम करने का आरोप है।
साल 2015 में पंजाब के बरगारी में गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान हुआ था। गुरुग्रंथ साबिह के अपमान के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में दो सिख युवकों की मौत हो गई थी।
कथित तौर पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के अनुयायियों पर अपमान करने के आरोप लगाए गए थे।
अक्तूबर में राम रहीम के ख़िलाफ़ अपमान के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही फिर से शुरू हुई।
साल 2007 में बठिंडा के सलबतपुरा में जुटे अपने अनुयायियों के बीच राम रहीम ने गुरु गोबिंद सिंह की नकल की थी। इस घटना के बाद डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों और सिखों के बीच झड़प हुई।
साल 2007 में अकाल तख़्त ने राम रहीम के बहिष्कार का आदेश जारी किया था।
यह सज़ा इस आरोप के तहत दी गई है कि 2007 में सिख समुदाय ने राम रहीम का बहिष्कार किया था इसके बावजूद अकाली नेतृत्व ने उनसे संबंध बनाए रखे। आरोप ये भी है कि कथित तौर पर बाद अकाली नेतृत्व ने अकाल तख्त की ओर से उन्हें माफ़ी दिलाने में मदद की।
सजा की घोषणा करते हुए जत्थेदार ने पार्टी की कार्यकारिणी को बादल का इस्तीफा स्वीकार करने और सदस्यता अभियान शुरू करने के लिए कमेटी के निर्माण की घोषणा करने को कहा।
दो दिसम्बर को अकाल तख़्त में क्या हुआ?
जत्थेदार अकाल तख़्त रघबीर सिंह और अन्य जत्थेदारों ने अकाल तख्त परिसर हाथ बांधे खड़े अकाली नेतृत्व से कई सवाल पूछे।
अकाल तख्त के मंच से खड़े होकर जत्थेदार रघबीर सिंह ने सुखबीर सिंह बादल से सात सवाल पूछे, जिसका उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया।
जत्थेदार ने पूछा, ‘सरकार में रहते हुए, क्या आपने सिखों की हत्या के लिए जि़म्मेदार अधिकारियों को पदोन्नति करने और उनके परिवारों को टिकट देने का पाप किया है? क्या आपने गुरमीत राम रहीम के मुकदमे को रद्द कराने का पाप किया है? क्या आपने अपने चंडीगढ़ के आवास पर जत्थेदारों को बुलाया और राम रहीम को माफी दिलाने का पाप किया है?’
उन्होंने आगे पूछा, ‘क्या आपने राम रहीम को माफी देने को सही ठहराने के लिए अखबारों में विज्ञापन देने के लिए एसजीपीसी फंड का दुरुपयोग करके पाप किया है?’
अकाली नेतृत्व से पूछा गया था कि क्या वे इन घटनाओं से वाकिफ़़ थे और इसके खिलाफ आवाज उठाई थी?
अकाली नेता किस तरह की सजा भुगत रहे हैं?
शिरोमणि अकाली दल के नेताओं की बात सुनने के बाद, अकाल तख़्त के जत्थेदारों और अन्य सिख प्रतिनिधियों ने फ़ैसले के लिए एक और बैठक की।
अकाल तख़्त मंच से खड़े होकर जत्थेदार रघबीर सिंह ने कहा, ‘अकाली नेताओं ने अपनी ग़लतियां स्वीकार कर ली हैं, इसलिए वे तीन दिसंबर से सेवा (तन्खा) करेंगे। वो दोपहर 12 से एक बजे तक स्वर्ण मंदिर परिसर के शौचालयों की सफाई करेंगे और दरबार साहिब प्रबंधक उनकी हाजिऱी लेंगे। इसके बाद स्नान कर बर्तन धोएंगे, गुरबाणी सुनेंगे और उसका पाठ करेंगे। इस दौरान वो गले में एक तख्ती भी लटकाएंगे।’
पैर में चोट के कारण सुखबीर और एक अन्य वरिष्ठ नेता सुखदेव सिंह ढींडसा के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उन्हें दो दिनों तक दो-दो घंटे व्हीलचेयर पर दरबार साहिब के द्वार पर बैठने, एसजीपीसी कर्मचारी की वर्दी पहनने और हाथों में भाला रखने की सज़ा सुनाई गई है।
ये दोनों नेता, पंजाब के दो अन्य तख़्तों और फतेहगढ़ साहिब के गुरुद्वारे में भी दो-दो दिन सेवा देंगे।
इसके अलावा, जत्थेदार ने एलान किया, ‘पूर्व जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह को दी गई सभी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी, जिन्होंने कथित तौर पर बादल परिवार के प्रभाव में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को माफ कर दिया था। उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों में बोलने की मनाही होगी।?
साथ ही उन्होंने सुखबीर बादल, सुच्चा सिंह लंगाह, गुलजार सिंह, दलजीत सिंह चीमा, बलविंदर सिंह भूंदड़ और हीरा सिंह गाबरिया से डेरा सच्चा सौदा से संबंधित विज्ञापनों पर खर्च किए गए धन की ब्याज सहित वसूली का भी निर्देश दिया।
दो दिसंबर को दिए गए फैसले में अकाल तख़्त ने 2011 में दिवंगत प्रकाश सिंह बादल को अकाल तख्त द्वारा दी गई पंथ रतन फख्र-ए-कौम की उपाधि भी वापस ले ली गई है। प्रकाश सिंह बादल पहले राजनेता थे जिन्हें यह उपाधि दी गई थी।
अकाल तख़्त क्या है और इसका सिख समुदाय के लिए क्या महत्व है?
दरबार साहिब सिखों की आध्यात्मिक शक्ति संस्था है, जबकि इस परिसर में बना अकाल तख़्त सिख समुदाय की स्वतंत्र पहचान का प्रतीक है।
सिखों के पांच तख़्त हैं- अकाल तख्त (अमृतसर), तख़््त केशगढ़ साहिब (आनंदपुर साहिब), तख्त दमदमा साहिब (तलवंडी साबो), तख्त श्री पटना साहिब (बिहार) और तख्त श्री नांदेड़ साहिब (महाराष्ट्र)।
सिखों के पांच तख़्तों में, अकाल तख़्त सबसे प्रमुख है और यह एकमात्र तख़्त है जिसे सिख गुरु ने स्थापित किया है।
अकाल तख्त को छठे गुरु, गुरु हरगोविंद साहिब ने खुद 15 जून 1606 में स्थापित किया था। इसका असली नाम अकाल बंगा था।
सिख धर्म की परम्पराओं के अनुसार, अकाल तख़्त का दजऱ्ा सबसे ऊपर है।
अकाल तख़्त की ओर से सिख़ों के लिए जारी किए जाने वाले आदेश को हुक्मनामा कहा जाता है, जिसका पालन करना हर सिख के लिए अनिवार्य है।
सजा सुनाने की क्या प्रक्रिया है?
चाहे कोई सिख कितना भी गणमान्य और शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह सिख धर्म के सिद्धांतों के ख़िलाफ़ जाता है, तो कोई भी सिख या संगठन उसकी शिकायत अकाल तख़्त से कर सकता है।
कोई मुद्दा आने पर अमृतसर के अकाल तख़्त सचिवालय में, अकाल तख़्त के जत्थेदार के नेतृत्व में पांच तख्तों के प्रतिनिधियों की बैठक होती है।
अगर किसी तख़्त का जत्थेदार इस बैठक में शामिल नहीं हो सकता है, तो उसके प्रतिनिधि के शामिल होने की उम्मीद की जाती है, या फिर दरबार साहिब (स्वर्ण मंदिर) के मुख्य ग्रंथी को बैठक में शामिल किया जा सकता है।
जत्थेदार बैठक में शिकायत पर विचार करते हैं और संबंधित व्यक्ति से सफाई मांगते हैं। अगर जत्थेदार उत्तर से संतुष्ट नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को दोषी घोषित कर दिया जाता है।
इसके बाद उस व्यक्ति को अकाल तख़्त के सामने पेश होने के लिए बुलाया जाता है। जत्थेदार अकाल तख़्त के मंच पर और आरोपी को संगत के सामने खड़ा किया जाता है।
अकाल तख़्त जत्थेदार संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आरोपों को पढ़ता है और उससे जवाब देने के लिए कहता है। अगर वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है या जत्थेदारों के अनुसार उस पर लगे आरोप सही साबित हो जाते हैं तो उसे धार्मिक सज़ा सुनाई जाती है।
अगर कोई व्यक्ति सज़ा स्वीकार नहीं करता या अकाल तख़्त के सामने हाजिर नहीं होता है तो उसे समुदाय से बहिष्कृत कर दिया जाता है।
लेकिन अगर व्यक्ति अपनी ग़लती स्वीकार कर लेता है और अकाल तख़्त के सामने हाजिऱ होता है, तो उसे धार्मिक दंड भी दिया जा सकता है और सिख समुदाय में बहाल भी किया जा सकता है।
अन्य सिख नेता जिन्हें धार्मिक सजा मिल चुकी है
1984 में ऑपरेशन ब्लूस्टार के बाद अकाल तख़्त की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई थी। बाद में भारत सरकार ने इसकी मरम्मत करवाई।
तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह और बुड्ढा दल के संता सिंह ने भारत सरकार की ओर से इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी ली थी।
सरकारी सहायता से बनी इस इमारत को सिखों ने मंजूरी नहीं दी और 1986 में सरबत खालसा (सिखों की बैठक) बुलाकर इसे गिराने का फैसला किया गया।
संता सिंह को सिख समुदाय से बहिष्कृत कर दिया गया और ‘तंखाहिया’ घोषित कर दिया गया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की थी और अकाल तख्त के सामने हाजिर हुए और उन्हें धार्मिक सज़ा कबूल की।
अकाल तख्त साहिब पर हमले के समय बूटा सिंह केंद्रीय गृह मंत्री थे और ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। दोनों माफी के लिए अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हुए थे।
2017 में पंजाब का विधानसभा चुनाव हारने के बाद 2018 में प्रकाश सिंह बादल खुद पूरे शिरोमणि अकाली दल नेतृत्व के साथ अकाल तख़्त के सामने हाजिर हुए और स्वर्ण मंदिर में जूते और बर्तन साफ करने की सेवा की। (bbc.com/hindi)
-जेम्स फिट्जगेराल्ड
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने बेटे हंटर बाइडन को प्रेसिडेंशियल पार्डन यानी राष्ट्रपति क्षमादान दिया है। हंटर दो आपराधिक मामलों में सज़ा का सामना कर रहे थे।
उनके इस कदम ने विवाद पैदा कर दिया है क्योंकि जो बाइडन ने पहले इस तरह का क्षमादान देने से इंकार कर दिया था। लेकिन उन्होंने तर्क किया कि उनके बेटे के खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित था।
अमेरिकी राजनीति के दोनों ध्रुवों से आने वाले राष्ट्रपतियों ने अपने कऱीबियों को क्षमादान देने के लिए राष्ट्रपति पद के विशेष अधिकार का इस्तेमाल किया है।
हंटर बाइडन ने क्या किया था?
हंटर बाइडन पर दो संघीय आपराधिक मामले चल रहे थे और उन्हें दोषी भी कऱार दिया गया था। इसी महीने के अंत में उन्हें सज़ा भी होने वाली थी।
बंदूक खऱीदने के मामले में हंटर बाइडन को जून में दोषी कऱार दिया गया था। अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति की संतान को किसी मामले में दोषी ठहराया गया है।
डेलावेयर में चल रहे मुक़दमे में हैंडगन खऱीदने के दौरान ड्रग इस्तेमाल को लेकर ग़लत जानकारी देने के सभी तीन आरोपों में उन्हें दोषी ठहराया गया था।
अमेरिका में बंदूक खऱीदते वक़्त झूठा बयान देने के लिए दस साल तक की सज़ा हो सकती है।
वहीं, यदि कोई व्यक्ति जिसे ड्रग्स लेने की लत हो, अवैध रूप से बंदूक रखता है तो उसे दस साल की सज़ा हो सकती है।
किसी संघीय लाइसेंसधारी बंदूक विक्रेता को बंदूक खरीदते वक्त झूठी जानकारी देने के आरोप में पांच साल तक की सजा होती है। यदि हंटर बाइडन को इन तीनों ही आरोपों में अधिकतम सजा दी जाती तो उन्हें 25 साल तक की सज़ा हो सकती थी।
बीते सितंबर में टैक्स चोरी के एक अन्य मामले में उन्होंने अपराध स्वीकार किया था और इस मामले में भी सज़ा होनी थी।
उन पर 2016 से 2019 के बीच टैक्स चोरी से जुड़े कुल 9 आरोप लगे थे जिनमें टैक्स रिटर्न और टैक्स न भरना और ग़लत रिटर्न भरना शामिल है।
टैक्स मामले में उन्हें अधिकतम 17 साल की सज़ा हो सकती थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा है कि हालांकि उनकी टैक्स देनदारी को कम करने और दोनों सजाओं के एक साथ होने की संभावना ज़्यादा थी।
राष्ट्रपति क्षमादान क्या है?
अमेरिकी संविधान के अनुसार, ‘राष्ट्रपति के पास महाभियोग को छोडक़र अमेरिका के खिलाफ किए गए किसी भी अपराध के लिए माफ़ी देने या सज़ा कम करने की व्यापक शक्ति होती है।’
इस मामले में ‘राष्ट्रपति की पूर्ण और बिना शर्त माफ़ी" दी गई है उसमें हंटर बाइडन को जनवरी 2014 से लेकर दिसम्बर 2024 के बीच किए गए सभी संघीय अपराधों में सज़ा से छूट मिल गई है।
यह एक ऐसी क़ानूनी माफ़ी है जो भविष्य में होने वाली किसी सज़ा को भी समाप्त कर देती है और वोट देने या सार्वजनिक पद की दौड़ में शामिल होने के अधिकारों को बहाल करती है।
हालांकि माफ़ी देने का अधिकार बहुत व्यापक माना जाता है और इसकी कोई सीमा नहीं होती है। हालांकि एक राष्ट्रपति केवल संघीय अपराधों के मामलों में ही माफ़ी जारी कर सकता है।
यह मुद्दा इस समय इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि एक पॉर्न फि़ल्म स्टार को चुपचाप भुगतान किए जाने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप की सज़ा पर भी संशय पैदा हो गया है।
हालांकि जब जनवरी में वह व्हाइट हाउस लौटेंगे तो प्रांतीय स्तर पर चल रहे इस मुकदमे में खुद को माफ़ी नहीं दे पाएंगे।
अब तक अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने कितने क्षमादान दिए हैं?
अमेरिका में दोनों ही पार्टियों से आने वाले राष्ट्रपतियों की ओर से अपने कऱीबियों को क्षमादान देने की लंबी परंपरा रही है। और डेमोक्रेट पार्टी से आने वाले बाइडन का राष्ट्रपति रहते हुए यह 26वां क्षमादान है।
साल 2020 में ट्रंप ने बेटी इवांका के पति और अपने दामाद चाल्र्स कुशनर को क्षमादान दिया था।
कुशनर को टैक्स चोरी, चुनाव प्रचार अभियान में वित्तीय अनियमितताओं और गवाही में दख़ल देने के आरोपों में 2004 में दो साल की जेल की सज़ा दी गई थी।
साल 2001 में बिल क्लिंटन ने अपने छोटे सौतेले भाई रोजर क्लिंटन को कोकेन से जुड़े अपराध में माफ़ी दी थी। हालांकि यह मामला 1985 का था।
इन दोनों मामलों में उन लोगों को क्षमादान दिया गया जो पहले ही सज़ा भुगत चुके थे। जबकि राष्ट्रपति बाइडन ने अपने बेटे के मामले में सज़ा होने से पहले ही दख़ल दिया है।
प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार, ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में अपने चार सालों के कार्यकाल दौरान 237 क्षमादान जारी किए, जिनमें 143 सज़ा माफ़ी और 94 सजाएँ कम की गई थीं। उनके पद छोडऩे से पहले कई लोग हड़बड़ाहट में थे। हालांकि ये ट्रंप के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा के मुकाबले फिर भी कम था।
प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक़, ओबामा ने अपने आठ साल के कार्यकाल में कुल 1,927 क्षमदान जारी किए था, जिनमें 1715 सज़ा में बदलाव और 212 सज़ा माफ़ी थी।
क्षमादान को लेकर ट्रंप ने क्या कहा?
क्षमादान को लेकर बाइडन की आलोचना करने वालों में नव निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप भी हैं। ट्रंप ने इसे ‘शक्तियों का दुरुपयोग और इंसाफ़ का गला घोंटना’ कऱार दिया।
ट्रंप ने पूछा कि क्या बाइडन उन लोगों को भी क्षमदान जारी करेंगे जिनपर 6 जनवरी 2021 के दंगे के मामले में मुकदमा चल रहा है।
ट्रंप के समर्थकों ने उस दिन अमेरिकी कैपिटल हिल इमारत पर हमला करके 2020 के चुनावी नतीजों को प्रमाणित करने में बाधा डालने की कोशिश की थी।
व्हाइट हाउस से बाहर रहते हुए ट्रंप को कई क़ानूनी मुकदमों का सामना करना पड़ा है और उन्होंने लगातार आरोप लगाए कि अमेरिकी न्याय तंत्र को उनके और उनके समर्थकों के ख़िलाफ़ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया।
उन्होंने वॉशिंगटन में हुए दंगे में शामिल लोगों को अपनी ओर से क्षमादान जारी करने का वादा किया था।
लेकिन किन्हें क्षमादान मिलेगा और गंभीर और हिंसक अपराधों में सज़ा पाए लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं, इस पर अभी भी सवाल है। (bbc.com/hindi)
भारत में पिछले कुछ महीनों से वक्फ को लेकर विवाद चल रहा है। दरअसल केंद्र सरकार दशकों पुराने वक्फ कानून को बदलना चाहती है। इसका देश में अलग-अलग जगहों पर विरोध हो रहा है।
विरोध करने वालों का कहना है कि सरकार बदलाव के विधेयक के बहाने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है।
जबकि सरकार की दलील है कि ये विधेयक वक्फ की संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल के लिए है।
प्रस्तावित विधेयक के जिन प्रावधानों पर आपत्ति है, उनमें से एक वक्फ काउंसिल के स्वरूप का भी है।
सेन्ट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्यों का मुसलमान होना जरूरी है लेकिन प्रस्तावित विधेयक में दो ग़ैर-मुसलमान सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान भी जोड़ दिया गया है।
इसके साथ ही सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल के मुसलमान सदस्यों में भी दो महिला सदस्यों का होना अनिवार्य कर दिया गया है।
नए वक्फ विधेयक के भारी विरोध के बाद, इसे एक संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया।
इस समिति के अध्यक्ष बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल हैं। अब इस समिति का कार्यकाल अगले साल होने वाले बजट सत्र तक बढ़ा दिया गया है।
तो क्या है वक्फ? क्या हैं वक्फ विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख संशोधन? क्यों है इस पर विवाद? सरकार क्यों इस पर इतना मुखर है और ये एक चुनावी मुद्दा कैसे बना हुआ है?
बीबीसी हिन्दी के साप्ताहिक कार्यक्रम, ‘द लेंस’ में कलेक्टिव न्यूजरूम के डायरेक्टर ऑफ जर्नलिज़्म मुकेश शर्मा ने वक्फ से जुड़े इन मुद्दों पर चर्चा की।
इस चर्चा में शामिल हुए- किताब ‘शिकवा-ए-हिंद: द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम’ के लेखक डॉक्टर मुजीबुर्रहमान, अबू धाबी से मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर जफ़ऱ सरेशवाला, बेंगलुरु से वरिष्ठ पत्रकार इमरान क़ुरैशी और वकील मुजीबुर्रहमान।
वक्फ क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई?
वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति होती है, जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति, अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद या परोपकार के मकसद से दान करता है।
ये संपत्ति परोपकार के मकसद से समाज के लिए दान दी जाती है।
अल्लाह के सिवा न तो इसका कोई मालिक होता है और न हो सकता है। न तो वक़्फ़ संपत्ति की खऱीद-फऱोख़्त की जा सकती है और न ही इन्हें किसी को हस्तांतरित किया जा सकता है।
वकील मुजीबुर्रहमान का मानना है कि वक्फ ट्रस्ट जैसा होता है। जिस तरह से ट्रस्ट में लोग संपत्ति दान कर देते हैं ठीक उसी तरह से इस्लाम में वक्फ़़ होता है।
मुजीबुर्रहमान कहते हैं, ‘इसमें कोई भी इंसान अपनी निजी संपत्ति को दीन के कामों के लिए या परोपकार के मकसद से वक्फकर देता है। जो भी इंसान संपत्ति वक्फ करते हैं वो अपने हिसाब से मुतवल्ली (वक्फ का ट्रस्टी) चुन सकते हैं।’
मुजीबुर्रहमान के मुताबिक वक्फ के पास 8 लाख 70 हजार ऐसी संपत्तियां हैं जिनकी पहचान हो चुकी हैं। साथ ही वक्फ के पास 9।50 लाख एकड़ ज़मीन है।
मुजीबुर्रहमान का कहना है कि वक्फ की 60 हजार जमीनें ऐसी है, जिन पर विवाद चल रहा है।
मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर जफर सरेशवाला बताते हैं ‘मोहम्मद पैगंबर मक्का से मदीना गए। इसे हम हिजरत कहते हैं।’
‘तब उन्होंने वहां सबसे पहले जो संस्थाएं क़ायम की वो थीं, पहला, औकाफ यानी वक्फ और दूसरा, बैतूल माल। दोनों का मकसद था कि भविष्य में अनाथों, विधवाओं, गरीबों की मदद की जाए।’
किस बात पर विवाद?
वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में प्रस्तावित संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। इसके बाद कई विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस पर नियंत्रण करना चाहती है।
सरकार ने इसमें कई बदलाव की बात कही है। प्रस्तावित संशोधन के तहत वक्फ की जमीन का सर्वे करने के अधिकार अतिरिक्त कमिश्नर के पास मौजूद होता है, इसे अब जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर को दे दिए गए हैं।
वक्फ बोर्ड में दो गैर मुसलमान प्रतिनिधि रखने का प्रावधान किया गया है। साथ ही दो महिला सदस्यों को भी शामिल करने की बात की गई है।
इस बिल के प्रावधान के अनुसार, वही व्यक्ति दान कर सकता है जिसने लगातार पांच साल तक इस्लाम का पालन किया हो यानी वो मुस्लिम हो और दान की जा रही संपत्ति का मालिकाना हक़ रखता हो।
पिछले दिनों केरल और कर्नाटक में वक्फ की संपत्तियों पर विवाद हुआ था। क्या इन दोनों राज्यों में ये मुद्दा सच में संवेदनशील है या राजनीतिक रूप से ज्य़ादा सक्रिय हुआ है?
वरिष्ठ पत्रकार इमरान कुरैशी का मानना है कि ये मामला राजनीतिक रूप से सक्रिय हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि केरल और कर्नाटक दोनों ही जगह उपचुनाव हो रहे थे।
वो कहते हैं कि किसानों को जो नोटिस भेजा गया वो सिर्फ कांग्रेस की सरकार में नहीं गए हैं, बल्कि बीजेपी की सरकार के समय में भी नोटिस भेजे गए थे।
वक्फ संपत्ति छिन जाने का डर
प्रस्तावित संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश होने का बाद से ही लोगों में इस बात का डर है कि सरकार उनकी जमीन को अपने कब्ज़े में लेना चाहती है।
लेकिन सरकार का दावा है कि इस बिल के आने से वक्फ संबंधित विवादों के निपटारे में आसानी होगी।
तो, क्या इस बिल से सरकार मुसलमानों के मामलों में अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती है?
इस पर ‘शिकवा-ए-हिंद’ द पॉलिटिकल फ्य़ूचर ऑफ़ इंडियन मुस्लिम’ के लेखक डॉक्टर मुजीबुर्रहमान का मानना है कि वक्फ में सुधार की ज़रूरत है।
मुजीबुर्रहमान का कहना है, ‘अगर मुस्लिम संपत्ति प्रबंधन में गैर-मुसलमान रह सकते हैं तो गैर-मुसलमानों के संपत्ति प्रबंधन में भी मुसलमानों को रहने की इजाजत होनी चाहिए।’
‘क्योंकि हिन्दुस्तान एक सेक्युलर देश है और यहां पर सबकी जिम्मेदारी है कि वो सभी चीज़ों की देखभाल करें।’
वकील मुजीबुर्रहमान का मानना है कि अगर वक्फ पर सरकार का नियंत्रण रहेगा तो फिर वो चीज कभी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। बल्कि सरकार अपना नुमाइंदा नियुक्त करके उन पर कब्ज़ा करेगी और अपने हिसाब से लोगों को जमीन देगी।
वो कहते हैं, ‘वक्फ को राजनीति से बाहर निकालना होगा, मुसलमानों को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह एक कमेटी बनानी होगी।’
‘वक्फ के सीईओ को सरकार को नहीं चुनना चाहिए, बल्कि वक्फ के खर्च पर इसके लिए चुनाव हो। ऐसा करने से ये राजनीति से बाहर होगा और मुसलमानों का इस पर नियंत्रण रहेगा।’
मुजीबुर्रहमान कहते हैं, ‘ये मामला पैसों का है, चाहे कोई भी सरकार हो हर कोई चाहती है उस चीज़ पर उनका कब्जा हो। डीएम सरकार का एक नुमाइंदा होता है। अगर उसको उस संपत्ति में एक फ़ीसदी भी विवाद नजऱ आएगा तो फिर वो संपत्ति सरकार की हो जाएगी।’
वहीं मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर जफऱ सरेशवाला इस पर कहते हैं कि वक्फ के पास इतनी संपत्ति है कि इसका इस्तेमाल सही से किया गया होता तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं इस देश का हिंदू भी गऱीब नहीं रहता।
वो कहते हैं, ‘उनका कहना है कि हज़ार करोड़ की संपत्ति संभालने के लिए ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी दस लाख की संपत्ति कभी न खऱीदी है और न कभी बेची है।’
‘हमें जरूरत है कि वहां ऐसे लोगों को बैठाया जाए जो बेहतर तरीक़े से इन संपत्तियों का ख्याल रख सकें।’
वक्फ कैसे बना चुनावी मुद्दा?
हाल में हुए दो राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ-साथ कई राज्यों की विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में वक्फ का मुद्दा गूंजता दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी इस दौरान इस मुद्दे को उठाती रही।
कर्नाटक में वक़्फ़ का मुद्दा हावी होने के बाद यहां की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में सभी पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की।
इमरान क़ुरैशी कहते हैं, ‘शायद इससे पहले कर्नाटक में मुतवल्लियों का चुनाव इस तरह से नहीं हुआ। इस चुनाव के लिए आज तक किसी भी मंत्री ने प्रचार नहीं किया था।’
‘लेकिन मंत्री जमीर अहमद खान ने हर तरफ जाकर प्रचार किया। इस दौरान वक्फ की ज़मीन का मुद्दा उठाया। इसकी वजह से बीजेपी ने इस मुद्दे को और भी उछाला।’
इमरान क़ुरैशी कहते हैं, ‘उपचुनाव में भी ये मुद्दा ज़ोर-शोर से चला, जिसके कारण जो हिंदू वोट एक होने वाला था वो नहीं होकर मुस्लिम, दलित और ओबीसी के वोट एक हो गए।’
‘इसी वजह से कांग्रेस तीनों सीटों पर जीत गई। लेकिन ये मामला अभी ख़त्म नहीं होगा ये आगे भी चलेगा।’
सरकार को क्या करने की ज़रूरत
वक्फ को लेकर लोगों के अलग-अलग दावे होते रहते हैं। जिसके बाद सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती हो जाती है कि वो लोगों को कैसे भरोसा दिलाए कि वो जो दलील दे रही है वो सही है।
इस पर डॉक्टर मुजीबुर्रहमान कहते हैं, ‘मुसलमानों में भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें वक़्फ़ की संपत्ति को लेकर क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है। क्यों मीडिया में इस खबर को सनसनीखेज़ बनाया जा रहा है।’
वो कहते हैं, ‘वक्फ में बहुत संपत्तियां विवादित हैं, तो बहुत सारी वैध भी हैं। इन सबको सामने लाने के लिए सुधार की ज़रूरत है। सरकार को एक वेबसाइट बनाकर लोगों तक सारी जानकारी पहुंचानी चाहिए।’
‘क्योंकि अयोध्या जजमेंट के बाद और बुलडोजऱ जस्टिस जिस तरह से चल रहा है, इससे कौम को ऐसा लग रहा है कि सरकार हमारी नहीं है, वो हमारी चीज़ें छीन रही है।’
‘इस सोच को कम करने के लिए सरकार को सक्रिय होकर सारी जानकारी इन लोगों को देनी होगी।’
लोगों के नज़रिए को बदलने के लिए वक्फ को क्या कदम उठाने चाहिए?
इस पर वकील मुजीबुर्रहमान कहते हैं कि जो फंड आ रहा है उसको लेकर सारी जानकारी पारदर्शी होनी चाहिए। ताकि लोग ये देख सके कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है।
वो कहते हैं, ‘ये लोगों की निजी संपत्तियां है, इस कारण जब तक कमेटी न चाहे, सरकार अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती।’
‘आज की तारीख़ में जो वक्फ बोर्ड है वो राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं क्योंकि सरकार ही उनके नुमाइंदों को नियुक्त करती है। इस कारण जैसी सरकार होगी बोर्ड उसके हिसाब से काम करेगा।’
‘वक्फ जो भी करता है वो मुलसमानों के लिए करता है, लेकिन अगर उस संपत्ति से सराय, हॉस्टल या कुछ और बना दिया जाए तो वो गैर-मुसलमान के लिए भी काम में आएगी।’ (bbc.com/hindi)
-फरहत जावेद
एक जली हुई लॉरी, जहां-तहां बिखरे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की तस्वीर वाले पोस्टर और आंसू गैस के फट चुके गोले। ये इमरान ख़ान की पत्नी बुशरा बीबी के नेतृत्व में हुए विशाल प्रदर्शन के बचे हुए निशान थे, जिसके बाद इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया गया था।
इसके एक दिन पहले, मंगलवार को दोपहर में बुशरा बीबी एक शिपिंग कंटेनर के ऊपर हिजाब पहने और सफेद शॉल ओढ़े अपने चिर-परिचित अंदाज़ में खड़ी थीं।
इस शिपिंग कंटेनर के आसपास विपक्षी पाकिस्तान तहरीक़-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) के हज़ारों समर्थक हाथों में इमरान ख़ान की तस्वीर और पार्टी का झंडा लिए खड़े थे और नारे लगा रहे थे।
वहां कानफाड़ू शोर था, लेकिन जैसे ही बुशरा बीबी ने माइक अपने हाथों में थामा, सन्नाटा पसर गया।
प्रदर्शन में क्या हुआ?
बुशरा बीबी ने चिल्लाकर कहा, ‘मेरे बच्चों और मेरे भाइयों! आपको मेरा साथ देना होगा।’
उनकी आवाज़ गूंजते ही भीड़ में हलचल शुरू हो गई और पूरे माहौल में एक बार फिर नारों की आवाज़ सुनाई देने लगी।
बुशरा बीबी ने अपनी बात जारी रखी और कहा, ‘लेकिन अगर आप लोग साथ नहीं भी रहते हैं, तो भी मैं मज़बूती से खड़ी रहूंगी। यह केवल मेरे पति का सवाल नहीं है, यह इस देश और इसके नेता का सवाल है।’
पाकिस्तान की राजनीति पर नजऱ रखने वाले कई जानकार इसे राजनीति में बुशरा बीबी की शुरूआत के तौर पर देख रहे हैं।
कुछ लोगों के लिए यह घटना राजनीति में उनका पहला कदम था। अन्य लोगों के लिए यह इमरान ख़ान की पीटीआई को तब तक बचाए रखने की रणनीतिक चाल थी, जब तक वो जेल में हैं।
बुशरा बीबी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की तीसरी पत्नी हैं और अक्सर उन्हें बेहद रिज़र्व माना जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो राजनीति से दूर रहती हैं।
लेकिन इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शनों के दौरान वो राजनीति के केंद्र में दिखीं।
लेकिन बुधवार सवेरे जब सूरज उगा, न तो बुशरा बीबी का कोई निशान मौजूद था और न ही उनके समर्थन में आए उन हज़ारों लोगों का जिन्होंने इमरान ख़ान की रिहाई के लिए मार्च में हिस्सा लिया।
शहर के अंधेरे में डूबने के बाद इस तथाकथित ‘फ़ाइनल मार्च’ और बुशरा बीबी के साथ क्या हुआ, ये अब तक स्पष्ट नहीं है।
एक महिला प्रदर्शनकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि अचानक बिजली चली गई और डी-चौक जहां विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, वो जगह अंधेरे में डूब गई।
2022 में हुए अविश्वास मत में इमरान ख़ान की सरकार गिर गई थी। इसके बाद अगस्त 2023 से इमरान ख़ान भ्रष्टाचार, चरमपंथ और हिंसा भडक़ाने के आरोप में जेल में हैं।
इमरान ख़ान खुद पर लगाए आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं।
फाइनल मार्च के दौरान अफरा-तफरी
महिला प्रदर्शनकारी ने बताया कि डी-चौक में हर तरफ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, वहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। वो अपने पति को पकड़ कर खड़ी थीं जिनके कंधे से गोली लगने के कारण ख़ून बह रहा था।
बाद में वो इस्लामाबाद के एक अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने बीबीसी उर्दू को बताया, ‘हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वो कयामत के दिन या युद्ध के दिन की तरह था।’
‘मेरे हाथों में मेरे पति का खूऩ लगा हुआ था और हर तरफ से चीखने की आवाज़ें आ रही थीं।’
लेकिन इतनी तेजी से अचानक क्या हुआ?
कुछ घंटों पहले, यानी मंगलवार की दोपहर को प्रदर्शनकारी डी-चौक पहुंचे। शहर के केंद्रीय हिस्से के इस इलाक़े तक पहुंचने के लिए उन्होंने बीते दिनों कई पुलिस बैरिकेडिंग पार की थी और आंसू गैस के गोले झेले थे।
इनमें पाकिस्तान तहरीक़-ए-इंसाफ़ के समर्थक और कार्यकर्ता शामिल थे।
जेल में रहते हुए इमरान ख़ान ने पार्टी समर्थकों से इस मार्च के लिए अपील की थी।
इस मार्च में लिए पीटीआई समर्थक और कार्यकर्ता इक_ा हुए और इस ‘फ़ाइनल मार्च’ में उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी शामिल हुईं और मार्च का नेतृत्व किया।
राजधानी की सडक़ों पर लाइन से बैरिकेड लगाए गए थे और पाकिस्तानी सेना का वहां कड़ा पहरा था।
जब काफिला शहर के कऱीब पहुंचा, बुशरा बीबी शिपिंग कंटेनर पर खड़ी समर्थकों का अभिवादन करती दिखाई दीं।
उन्होंने एलान किया, ‘जब तक ख़ान हमारे पास नहीं आते, हम वापस नहीं जाएंगे।’
यह मार्च आगे बढ़ता हुआ इस्लामाबाद के सरकारी कार्यालयों वाले उस इलाक़े में पहुंच गया, जिसे डी-चौक कहते हैं।
पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, पार्टी के भीतर मतभेद और प्रदर्शन के लिए अन्य जगह चुनने की सरकार की अपील के बावजूद बुशरा बीबी ने उस इलाके में प्रदर्शन करने का चुनाव किया जहां संसद, प्रमुख सरकारी कार्यालय स्थित हैं। इस इलाक़े में उनके पति इमरान ख़ान एक बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं।
बुशरा बीबी का ग़ायब होना
जैसे ही दिन ढला, हालात तनावपूर्ण हो गए। इलाके की बिजली गुल हो गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। इसके बाद स्थानीय समयानुसार रात के साढ़े नौ बजे सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेडऩे के लिए अभियान चलाया।
इस दौरान मची अफरा-तफरी के बीच बुशरा बीबी धरना स्थल से चली गईं।
सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हुए जिसमें वो इलाक़े से बाहर जाते हुए एक कार से दूसरे कार में बैठती दिखाई दीं। बीबीसी इन फुटेज की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर पाया है।
जिस वक्त समर्थक आंसू गैस के गोलों और गिरफ़्तारियों का सामना कर रहे थे ऐसे में उनके वहां से अचानक ग़ायब होने ने कई लोगों को निराश किया।
कुछ देर बाद जिस शिपिंग कंटेनर पर वो दिखाई दी थीं, उसे अज्ञात लोगों ने आग के हवाले कर दिया।
एक व्यक्ति ने कहा, ‘उन्होंने हमें छोड़ दिया।’
एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ‘उनकी गलती नहीं थी। पार्टी के नेताओं ने उन्हें वहां से जाने को मजबूर किया।’
राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार मेहमाल सरफराज ने कहा, ‘उनके अचानक ग़ायब होने से, उनका राजनीतिक करियर के शुरू हो इससे पहले नुकसान हो गया।’ हालांकि कुछ वक्त पहले इमरान ख़ान ने सोशल मीडिया पर लिखा था, ‘मेरी पत्नी केवल मेरा संदेश लोगों तक पहुंचातीं’ हैं।
रात के एक बजे के आसपास प्रशासन ने कहा कि प्रदर्शनस्थल से सभी लोग जा चुके हैं।
इस दौरान कितने लोगों को चोटें आई या कितनों की मौत हुई, इस बारे में अब तक आधिकारिक रूप जानकारी साझा नहीं की गई है। हालांकि बीबीसी ने स्थानीय अस्पतालों से बात कर पुष्टि की है कि इसमें कम से कम पांच लोगों की जान गई है।
पुलिस का कहना है कि रात को कम से कम 500 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस स्टेशन में रखा गया है। वहीं पीटीआई का दावा है कि कई लोग लापता हैं।
इमरान ख़ान से शादी
पाकिस्तान के अपेक्षाकृत संपन्न पंजाब प्रांत के प्रभावशाली ज़मींदार परिवार से आने वाली बुशरा बीबी की शादी इमरान ख़ान से 2018 में हुई थी। इसे लेकर उस वक्त मिली-जुली प्रतिक्रिया रही थी।
इससे पहले वो 28 साल तक विवाहित जीवन बिता चुकी थीं। उनके पूर्व पति ने उन पर इस्लामिक क़ानूनों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि तलाक और फिर से शादी करने के बीच पर्याप्त समय नहीं लिया गया। उनका कहना था कि यह इस्लामिक कानूनों का उल्लंघन है।
इस मामले में इमरान ख़ान और बुशरा बीबी को सज़ा हुई लेकिन बाद में बरी कर दिया गया।
बुशरा बीबी सूफ़ी पंथ में आस्था रखती हैं और पार्टी के करीबी लोगों का मानना है कि पर्दे के पीछे इमरान खान को सलाह देने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। इमरान खान उन्हें आध्यामिक गुरु मानते हैं।
लेकिन पीटीआई की राजनीति में उनका सार्वजनिक रूप से शामिल होना नया और विवादित भी है।
इसी महीने की शुरुआत में वो ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह की राजधानी पेशावर में हुई पार्टी की एक बैठक में शामिल हुईं, जहां पीटीआई की सरकार है।
इसी बैठक में उन्होंने पार्टी नेताओं से इस फ़ाइनल मार्च में शामिल होने की बात की। उन्होंने ऐसा न करने पर नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी थी, जिसमें पार्टी से निकाला जाना भी शामिल था।
कुछ लोग इसे उनके बढ़ते प्रभाव के रूप में भी देखते हैं। जबकि कुछ लोग इसे पार्टी में हस्तक्षेप मानते हैं।
पत्रकार आमिर जिय़ा ने कहा, ‘उनका यह नज़रिया पीटीआई के नेताओं को रास नहीं आया।’
‘पार्टी खुद ही वंशवादी राजनीति का विरोध करती आई है। अगर वो आधिकारिक भूमिका अख़्तियार करती हैं तो यह पार्टी और इमरान ख़ान दोनों की छवि को नुक़सान पहुंचा सकती है।’
बुशरा बीबी और राजनीति में उनका कदम
राजनीतिक विश्लेषक इम्तियाज़ गुल ने बीबीसी उर्दू से कहा कि राजनीति में उनका शामिल होना ‘असाधारण हालात में उठाया गया असाधारण कदम’ है।
उन्होंने कहा, ‘असल में यह इमरान ख़ान की ग़ैर मौजूदगी में पार्टी और पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की कोशिश थी।’
पीटीआई के कुछ सदस्य भी यही कहते हैं। उनका मानना है कि ‘वो राजनीति में केवल इसलिए आई हैं क्योंकि इमरान ख़ान उन पर पूरा भरोसा करते हैं।’
लेकिन पार्टी के भीतर दबी आवाज़ में इस तरह की बातें होती रही हैं कि इमरान ख़ान जब प्रधानमंत्री थे, उस वक्त उनके फ़ैसलों को बुशरा बीबी प्रभावित करती थीं।
हालांकि पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में ऐसा करने वाली वह पहली महिला नहीं हैं। इससे पहले भी देश में होने वाले कई प्रदर्शनों और रैलियों की अगुवाई महिलाएं कर चुकी हैं, खासकर तब जब उनके पति को गिरफ़्तार किया गया या उन पर आरोप लगाए गए।
पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ज़ुल्फिक़ार अली भुट्टो की पत्नी नुसरत भुट्टो और तीन बार के प्रधानमंत्री रहे नवाज़ शरीफ़ की पत्नी कलसुम नवाज़ तब सुर्खियों में आईं जब उनके पतियों को जेल हुई थी।
इस महीने की शुरूआत में पहली बार बुशरा बीबी ने उस वक्त सीधे-सीधे राजनीति में कदम रखने का एलान किया जब उन्होंने इमरान ख़ान के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए पीटीआई के आला नेताओं की बैठक की अपील की।
हालांकि प्रदर्शन के दो सप्ताह पहले उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा था कि उनका ‘राजनीति में आने का उनका इरादा नहीं है।’
कुछ लोग उनके इस दावे को संदेह से देखते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख़्वाजा आसिफ़ ने बुशरा बीबी पर अवसरवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि ‘वह भविष्य में खुद को नेता के रूप में देखती हैं।’
हालांकि पीटीआई के अंदर ही इस मामले में मतभेद हैं। कुछ लोगों ने बीबीसी को बताया कि ‘इमरान ख़ान उन पर बहुत भरोसा करते हैं।’ जबकि कई लोग इस बात से चिंतित हैं कि उनके शामिल होने से पार्टी के लोकतांत्रिक मूल्यों को नुक़सान पहुंचेगा।
इमरान ख़ान बुशरा बीबी पर कितना भरोसा करते हैं, इस बारे में राजनीतिक विश्लेषक मेहमाल सरफऱाज़ कहते हैं, ‘पीटीआई में इमरान ख़ान की बात ही अंतिम होती है। लेकिन राजनीति में शामिल होने की महत्वाकांक्षा रखने वाली उनकी दूसरी पत्नी रेहम ख़ान के उलट बुशरा बीबी का क़द और प्रभाव अधिक है।’
उनके मुताबिक़, ‘ऐसा इसलिए है क्योंकि इमरान ख़ान बुशरा बीबी को अपने आध्यात्मिक गुरू के रूप में देखते हैं। यही बात बुशरा बीबी को उनकी बाकी पत्नियों से अलग करती है।’
पत्रकार आमिर जिय़ा का मानना है कि पीटीआई समर्थकों को इस्लामाबाद तक मार्च करने के लिए प्रोत्साहित करने का बुशरा बीबी का ‘दांव उलटा’ पड़ गया। (बाकी पेज 8 पर)
इन आलोचनाओं के बावजूद, कई पीटीआई समर्थक बुशरा बीबी को इमरान ख़ान की कऱीबी मानते हैं।
इस्लामाबाद के रहने वाले आसीम अली कहते हैं, ‘वो उन लोगों में हैं जो असल में इमरान ख़ान की रिहाई चाहते हैं। मुझे उन पर पूरी तरह भरोसा है।’
लेकिन एक बात साफ़ है कि पहले की तरह बुशरा बीबी की शख़्सियत अब रहस्यमयी नहीं रह गई है। अब वो पाकिस्तान की राजनीति के केंद्र में हैं- चाहे वो ऐसा चाहती रही हों या नहीं।
(जोएल गुन्टो और युवेट टैन की अतिरिक्त रिपोर्टिंग के साथ)
द्वारिका प्रसाद अग्रवाल
मेरी अम्मा के पति और श्वसुर दोनों अद्भुत प्राणी थे। अम्माजी भोजन बनाने में अपने प्राण भी लगा दे तो भी उनको स्वाद नहीं आता था, खाते जाते थे, दांत पीसते जाते थे और थाली-गिलास पटक कर अपना क्रोध प्रगट करते रहते, बेचारी अम्मा चुपचाप सुनती-सहती रहती। हमारे घर में रोज दो-चार मेहमानों का भोज होता था, समाज में दोनों बाप-बेटे की मेहमाननवाज़ी की तारीफ हुआ करती थी, अम्माजी की बदौलत। बेचारी चूल्हे की आग में तपती भोजन बनाती, अकेले परोसती-खिलाती और सब खानेवाले मुंह पोछते हुए बिना कुछ कहे चले जाते। जिस भोजन के स्वाद पर दोनों बाप-बेटे अम्माजी को गरियाते थे, उस भोजन को याद करके आज हम तरसते हैं।
अम्माजी लाजवाब भोजन बनाती थी। चूल्हे में लकड़ी जलाकर बटुवे में पकी दाल और भात का स्वाद आज भी मुझे याद है। रोटी और पूरी को ऐसा गोल बेलती कि 'सर्कुलेटर' से 'चेक' कर लो। उनमें गजब की फुर्ती थी, रोटी सेंकते हर समय उनकी एक रोटी तवे पर होती, दूसरी अंगार पर और तीसरी पटे पर ! उनके हाथ से सिंकी हुई रोटियों की मुलायमियत अब स्मृति-शेष होकर रह गई। फूली हुई पूरियां और रसीली आलू या लौकी की सब्जी आज भी बहुत याद आती हैं। उनके हाथ से बने पापड़, बिजौरा, बड़ी, कचरिया, अथान (अचार) अब कहाँ ? मूंग और बेसन के लड्डू का वह सोंधापन, गुझिया और इन्दरसा की मिठास और प्रसव के पश्चात प्रसूता को खिलाए जाने वाले मेवा-मसालेदार 'सोंठइला लड्डू' का स्वाद न जाने कहाँ विलीन हो गया !
अम्माजी की याद में कितनी घटनाएँ मेरे ज़ेहन में उमड़ रही हैं, उन सब यादों को जोडक़र यदि उनका व्यक्तित्व परिभाषित किया जाए तो वे अत्यंत परिश्रमी और सरल स्वभाव की महिला थी। उनकी सरलता ने उनको बहुत सताया और जिस मान-सम्मान की वे हकदार थी, वह उन्हें नहीं मिला।
अम्माजी और दद्दाजी विपरीत स्वभाव वाले युगल थे, एक आग का गोला तो दूसरा बर्फ की चट्टान! लेकिन दद्दाजी तो दद्दाजी थे, उनके स्वभाव का क्या कहने ?
मैंने देखा है कि सीधे-सरल स्वभाव के व्यक्ति के साथ हमेशा अन्याय होता है। मनुष्य को फुफकारने वाले नाग की तरह जीवनशैली अपनानी चाहिए ताकि लोग उससे भयभीत रहें, यदि आप पिटपिटिया साँप के तरह अपना बचाव करते रहेंगे तो लोग आपको पैरों से कुचलते रहेंगे, आपको अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ।
( आत्मकथा का एक अंश)
अफ़सरों ने मोदी को लिखा, मिलने का वक़्त माँगा
प्रिय प्रधानमंत्री जी,
हम स्वतंत्र नागरिकों का एक समूह हैं, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में देश में बिगड़ते सांप्रदायिक संबंधों को सुधारने के लिए प्रयास किए हैं। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि पिछले एक दशक में समुदायों, विशेष रूप से हिंदुओं और मुसलमानों तथा कुछ हद तक ईसाइयों के बीच संबंध अत्यधिक तनावपूर्ण रहे हैं, जिससे ये दोनों समुदाय अत्यधिक चिंता और असुरक्षा में हैं।
वर्तमान परिस्थितियों में हमारे पास आपसे सीधे बात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, हालांकि हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप मौजूदा परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं।
ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिक संबंध हमेशा अच्छे रहे हों। विभाजन की भयावह यादें, उसके लिए जिम्मेदार परिस्थितियां और उसके बाद हुए दुखद दंगे हमारे दिमाग में अभी भी बसे हुए हैं। हम यह भी जानते हैं कि विभाजन के बाद भी हमारे देश में समय-समय पर भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और अब स्थिति पहले से बेहतर या बदतर नहीं है। हालांकि, पिछले दस वर्षों की घटनाएं इस मायने में काफी अलग हैं कि वे संबंधित राज्य सरकारों और उनके प्रशासनिक तंत्र की स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण भूमिका को दर्शाती हैं। हमारा मानना है कि यह अभूतपूर्व है। गोमांस ले जाने के आरोप में मुस्लिम युवकों को धमकाने या पीटने की घटनाओं से शुरू हुई यह घटना निर्दोष लोगों की उनके घरों में ही हत्या करने और उसके बाद स्पष्ट रूप से नरसंहार के इरादे से इस्लामोफोबिक नफरत भरे भाषणों में बदल गई। हाल के दिनों में मुस्लिम व्यापारिक प्रतिष्ठानों और भोजनालयों का बहिष्कार करने, मुसलमानों को परिसर किराए पर न देने और स्थानीय प्रशासन के नेतृत्व में मुख्यमंत्रियों के इशारे पर मुस्लिम घरों को बेरहमी से गिराने के आह्वान किए गए हैं। प्रेस में बताया गया है कि लगभग 154,000 प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं या अपने व्यवसाय के स्थान से वंचित हो गए हैं। इनमें से अधिकांश मुसलमानों के हैं।
ऐसी गतिविधि वास्तव में अभूतपूर्व है और इसने न केवल इन अल्पसंख्यकों बल्कि वास्तव में यहां और विदेशों में सभी धर्मनिरपेक्ष भारतीयों के आत्मविश्वास को हिला दिया है।
जैसे कि ये घटनाएं पर्याप्त नहीं थीं, नवीनतम उकसावे की वजह अज्ञात सीमांत समूह हैं, जो हिंदू हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं और उन स्थलों पर प्राचीन हिंदू मंदिरों के अस्तित्व को साबित करने के लिए मध्ययुगीन मस्जिदों और दरगाहों पर पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग कर रहे हैं। पूजा स्थल अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, न्यायालय भी ऐसी मांगों पर अनावश्यक तत्परता और जल्दबाजी के साथ प्रतिक्रिया करते दिखते हैं।
उदाहरण के लिए, यह अकल्पनीय लगता है कि एक स्थानीय न्यायालय सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 12वीं सदी की दरगाह पर सर्वेक्षण का आदेश दे - जो न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि उन सभी भारतीयों के लिए एशिया में सबसे पवित्र सूफी स्थलों में से एक है, जिन्हें हमारी समन्वयवादी और बहुलवादी परंपराओं पर गर्व है। यह सोचना ही हास्यास्पद है कि एक भिक्षुक संत, एक फकीर जो भारतीय उपमहाद्वीप के अद्वितीय सूफी/भक्ति आंदोलन का अभिन्न अंग था, और करुणा, सहिष्णुता और सद्भाव का प्रतिरूप था, अपने अधिकार का दावा करने के लिए किसी भी मंदिर को नष्ट कर सकता है। वास्तव में, आप सहित लगातार प्रधानमंत्रियों ने शांति और सद्भाव के उनके संदेश के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर 'चादरें' भेजी हैं। इस अद्वितीय समन्वयकारी स्थल पर वैचारिक हमला हमारी सभ्यतागत विरासत पर हमला है और समावेशी भारत के उस विचार को विकृत करता है जिसे आप स्वयं पुनर्जीवित करना चाहते हैं।
महोदय, ऐसी गड़बड़ियों के सामने समाज प्रगति नहीं कर सकता और न ही विकसित भारत का आपका सपना साकार हो सकता है।
हम चिंतित नागरिक जिन्होंने भारत सरकार के लिए यहां और विदेशों में विभिन्न क्षमताओं में काम करते हुए अपना जीवन समर्पित किया है, मानते हैं कि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो सभी अवैध, हानिकारक गतिविधियों को रोक सकते हैं। इसलिए, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सुनिश्चित करें कि मुख्यमंत्रियों और उनके अधीन प्रशासन कानून और भारत के संविधान का पालन करें, और अपने कर्तव्यों में किसी भी तरह की लापरवाही से अनगिनत दुखों का सामना करना पड़ेगा।
आपकी अध्यक्षता में एक सर्वधर्म बैठक की तत्काल आवश्यकता है जहां आपको एक समावेशी भारत के प्रधान मंत्री के रूप में यह संदेश देना चाहिए कि भारत सभी के लिए एक भूमि है, जहां सदियों से सभी धर्म एक साथ और सद्भाव में मौजूद हैं और किसी भी सांप्रदायिक ताकतों को इस अद्वितीय बहुलवादी और विविध विरासत को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महोदय, समय की बहुत कमी है और हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सभी भारतीयों, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों को आश्वस्त करें कि आपकी सरकार सांप्रदायिक सौहार्द, सद्भाव और एकीकरण को बनाए रखने के अपने संकल्प पर अडिग रहेगी।
हम यह भी अनुरोध करते हैं कि यदि हमारे बीच से एक छोटे प्रतिनिधिमंडल को आपसे मिलने का समय दिया जाए।
धन्यवाद,
भवदीय
1: एन. सी. सक्सेना: आईएएस (सेवानिवृत्त): पूर्व सचिव, भारत के योजना आयोग
2: नजीब जंग: आईएएस (सेवानिवृत्त): पूर्व उपराज्यपाल, दिल्ली
3: शिव मुखर्जी, आईएफएस (सेवानिवृत्त): ब्रिटेन में भारत के पूर्व उच्चायुक्त
4: अमिताभ पांडे: आईएएस (सेवानिवृत्त): पूर्व सचिव, अंतर-राज्य परिषद, भारत सरकार
5: एस.वाई. क़ुरैशी: आईएएस (सेवानिवृत्त): भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त
6: नवरेखा शर्मा: आईएफएस (सेवानिवृत्त): इंडोनेशिया में भारत के पूर्व राजदूत
7: मधु भादुड़ी: आईएफएस (सेवानिवृत्त): पुर्तगाल में पूर्व राजदूत
8: लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह (सेवानिवृत्त): पूर्व थल सेनाध्यक्ष
9: रवि वीरा गुप्ता: आईएएस (सेवानिवृत्त): पूर्व उप. गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
10: राजू शर्मा: आईएएस (सेवानिवृत्त): पूर्व सदस्य, राजस्व बोर्ड, सरकार। उत्तर प्रदेश के
11: सईद शेरवानी: उद्यमी/परोपकारी
12: अवय शुक्ला: आईएएस (सेवानिवृत्त): पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार
13: शाहिद सिद्दीकी: पूर्व संपादक, नई दुनिया
14: सुबोध लाल: आईपीओएस ( इस्तीफा दे दिया): पूर्व उप महानिदेशक, संचार मंत्रालय, भारत सरकार
15: सुरेश के. गोयल: आईएफएस (सेवानिवृत्त): पूर्व महानिदेशक, आईसीसीआर
16: अदिति मेहता: आईएएस (सेवानिवृत्त): पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, सरकार। राजस्थान
17: अशोक शर्मा: आईएफएस (सेवानिवृत्त): फिनलैंड और एस्टोनिया में पूर्व राजदूत
(मूल चिट्ठी इंग्लिश में है, 'छत्तीसगढ़' अख़बार ने इसे गूगल से अनुवाद किया है)
-सौतिक बिस्वास
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के अनुसार, सितंबर महीने में समाप्त हुए अमेरिकी वित्तीय वर्ष 2024 में, चार्टर्ड और कॉमर्शियल उड़ानों के ज़रिए एक हज़ार से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा गया है।
अक्तूबर 2020 से अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीपीबी) के अधिकारियों ने उत्तर और दक्षिण दोनों सीमाओं पर अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले करीब 1 लाख 70 हज़ार भारतीयों को हिरासत में लिया है।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को लेकर सख़्त नीति अपनाने का वादा किया है। ट्रंप 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति का पद संभालने वाले हैं।
अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने के कई जोखिम हैं। चाहे कजऱ् लेकर भारत छोडऩा हो, ख़तरनाक सफऱ में जान गंवाने का ख़तरा हो या फिर अमेरिका में क़ानून का सामना करना हो। फिर भी बड़ी संख्या में भारत के लोग यह जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटते हैं।
इसी अक्तूबर महीने में अमेरिका के इमिग्रेशन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) विभाग ने भारतीय नागरिकों को वापस घर भेजने के लिए एक चार्टर्ड विमान भेजा। जिससे अमेरिका से लोगों को वापस भारत में निर्वासित करने के बढ़ते ट्रेंड का संकेत मिलता है।
यह कोई सामान्य फ़्लाइट नहीं थी। यह इस साल बड़े पैमाने पर रवाना की जाने वाली ‘निष्कासन उड़ानों’ में से एक थी, जिनमें से हर फ़्लाइट में आमतौर पर 100 से अधिक लोग सवार थे।
ये उड़ानें उन भारतीय प्रवासियों को वापस ला रही थीं, जिनके पास ‘अमेरिका में रहने के लिए कोई कानूनी अधिकार नहीं था।’
अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक़, वयस्क पुरुषों और महिलाओं को लेकर आने वाली सबसे ताज़ा उड़ान पंजाब के लिए रवाना हुई, जो कई निर्वासित लोगों के मूल निवास के कऱीब है। हालाँकि इनके मूल निवास के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई।
अवैध भारतीयों की बड़ी तादाद
इस वित्तीय वर्ष में अमेरिका से भारत भेजे गए अवैध प्रवासियों के बारे में अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के सहायक सचिव रॉयस बर्नस्टीन मरे ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, ‘यह पिछले कुछ साल में अमेरिका से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने में लगातार हो रही बढ़ोतरी का हिस्सा है, जो पिछले कुछ साल में भारतीय नागरिकों के साथ हुई मुठभेड़ों में हो रही सामान्य बढ़ोतरी के मुताबिक़ है।’
यहां मुठभेड़ का मतलब उन घटनाओं से है, जिसमें लोगों को मेक्सिको या कनाडा की तरफ से अमेरिकी सीमा को अवैध तरीके से पार करने की कोशिश के दौरान अमेरिकी अधिकारी रोकते हैं।
जैसे-जैसे अमेरिका भारतीय नागरिकों की वापसी को बढ़ा रहा है, इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों का इस पर क्या असर होगा।
ट्रंप ने पहले ही अमेरिका के इतिहास में प्रवासियों के सबसे बड़े निर्वासन का वादा किया है।
वॉशिंगटन स्थित थिंकटैंक निस्केनन सेंटर के इमिग्रेशन विश्लेषक गिल गुएरा और स्नेहा पुरी कहते हैं, ‘भारतीयों की संख्या हालांकि लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों से आने वाले लोगों की तुलना में कम है, लेकिन पिछले चार साल में सीपीबी का सामना जिन लोगों से हुआ है उनमें पश्चिमी गोलार्ध के बाहर से आने वाले प्रवासियों में भारतीय नागरिक सबसे ज़्यादा हैं।’
थिंकटैंक प्यू रिसर्च सेंटर के शोध के नए आंकड़े बताते हैं कि अनुमान के मुताबिक़ साल 2022 तक अमेरिका में सवा 7 लाख ऐसे भारतीय थे, जिनके पास वहाँ रहने के लिए वैध दस्तावेज़ नहीं थे। यह मेक्सिको और अल सल्वाडोर के नागरिकों के बाद तीसरी सबसे बड़ी तादाद है।
कुल मिलाकर अवैध प्रवासी अमेरिका की कुल आबादी का 3 फ़ीसदी और विदेश में जन्मे अमेरिकी लोगों की आबादी का 22 फ़ीसदी हिस्सा हैं।
आंकड़ों पर गौर करें तो गुएरा और पुरी ने भारतीय नागरिकों के अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिशों में बढ़ोतरी के ट्रेंड को जानने की कोशिश की है।
अवैध तरीका अपनाने की वजह
पहली वजह
ऐसे प्रवासी जो अवैध तरीक़े से अमेरिका में बसना चाहते हैं वो निम्न आय वर्ग से नहीं आते, लेकिन वो अक्सर कम शिक्षा या अंग्रेज़ी में बात नहीं कर पाने की वजह से अमेरिका के लिए पर्यटक या छात्र वीज़ा हासिल नहीं कर पाते।
इसके बजाय ऐसे लोग उन एजेंसियों पर निर्भर रहते हैं जो एक लाख डॉलर तक पैसे वसूलते हैं और कभी-कभी सीमा की निगरानी करने वालों को चकमा देने के लिए बनाए गए लंबे और मुश्किल रास्तों का इस्तेमाल करते हैं।
इस रकम के लिए कई लोग अपने खेत भी बेच देते हैं या कजऱ् ले लेते हैं। यह हैरानी की बात नहीं है कि साल 2024 में अमेरिकी इमिग्रेशन अदालतों के आंकड़ों से पता चलता है कि ज़्यादातर अवैध भारतीय प्रवासी 18-34 साल के पुरुष थे।
दूसरी वजह
इस मामले से जुड़ी दूसरी बात यह है कि उत्तरी सीमा पर कनाडा जाना भारतीयों के लिए अमेरिका में प्रवेश के लिहाज से ज़्यादा आसान है, जहां विजि़टर्स वीज़ा के प्रोसेस का समय 76 दिन का है, जबकि भारत में अमेरिकी वीज़ा के लिए एक साल तक का समय लगता है।
स्वैंटन सेक्टर अमेरिका के उत्तर-पूर्व में मौजूद वर्मोंट राज्यों, न्यूयॉर्क और न्यू हैंपशर की काउंटियों को कवर करता है।
शोधकर्ताओं ने पाया कि इस साल की शुरुआत से ही इन इलाक़ों में सीमा पर मौजूद अधिकारियों का भारतीय नागरिकों के साथ सामना होने की घटना में अचानक बढ़ोतरी हुई है। यह जून महीने में 2715 तक पहुंच गई।
इससे पहले ज़्यादातर अनियमित भारतीय प्रवासी अल सल्वाडोर या निकारागुआ के रास्ते से मेक्सिको के साथ व्यस्त दक्षिणी सीमा से अमेरिका में प्रवेश करते थे। ये दोनों ही प्रवास को सुविधाजनक बनाते थे।
पिछले साल नवंबर तक भारतीय नागरिकों को अल सल्वाडोर में वीज़ा-मुक्त यात्रा की सुविधा मिल रही थी।
गुएरा और पुरी कहते हैं, ‘अमेरिका-कनाडा सीमा, अमेरिका-मेक्सिको सीमा से भी ज़्यादा लंबी और कम निगरानी वाली है। हालांकि यह ज़रूरी नहीं है कि यह रूट ज़्यादा सुरक्षित हो, लेकिन यहां आपराधिक समूहों की मौजूदगी उतनी नहीं है, जितनी दक्षिण और मध्य अमेरिका के रूट पर है।’
रोजग़ार की तलाश
ऐसा लगता है कि अमेरिका में अधिकांश प्रवासी सिख-बहुल राज्य पंजाब और पड़ोसी हरियाणा से आते हैं। इन राज्यों के लोग पारंपरिक रूप से विदेश जाते रहे हैं। ऐसे लोगों का दूसरा मूल स्रोत गुजरात है, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है।
तीसरी वजह
पंजाब राज्य जहां से अनियमित भारतीय प्रवासियों की एक बड़ी संख्या आती है। यह राज्य बेरोजग़ारी के बढ़ते स्तर, कृषि संकट और नशीले पदार्थों के सेवन की बढ़ती समस्या सहित आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है।
पंजाबियों में प्रवास भी लंबे समय से आम बात रही है और राज्य के ग्रामीण युवा आज भी विदेश जाने के लिए उत्सुक रहते हैं।
पंजाब में नवजोत कौर, गगनप्रीत कौर और लवजीत कौर ने 120 लोगों पर किए एक हालिया सर्वे में पाया कि 18-28 साल के 56त्न लोग आमतौर पर माध्यमिक शिक्षा के बाद प्रवास कर गए।
कई लोग कजऱ् लेकर विदेश में बस गए और बाद में अपने परिवार को पैसे भेजे।
उसके बाद राज्य में अलगाववादी सिख आंदोलन की वजह से तनाव बढ़ गया है, जो सिखों के लिए एक आज़ाद देश बनाना चाहता है।
पुरी कहती हैं, ‘इससे भारत के कुछ सिखों में यह डर पैदा हो गया कि उन्हें अधिकारी या नेता ग़लत तरीके से निशाना बना सकते हैं। यह डर उत्पीडऩ के दावों के लिए एक विश्वसनीय आधार भी मुहैया कर सकता है, जो उन्हें शरण मांगने की वजह देता है, चाहे वह सच हो या नहीं।’ हालाँकि भारतीयों के पलायन के पीछे पक्की वजहों का पता लगाना आसान नहीं है।
पुरी कहती हैं, ‘लोगों के लिए विदेश में बसने की इच्छा के पीछे अलग-अलग वजहें हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर विदेशों में ज़्यादा मौक़े मिलना इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है। साथ ही समाज में अमेरिका में 'बसने' की गर्व की भावना भी अहम है।’
बेहतर अवसर और ख़तरा
शोधकर्ताओं ने पाया कि विदेशों में बसने की वजह यह है कि सीमा पर भारतीय नागरिकों के स्वरूप में बदलाव आया है।
ज़्यादातर परिवार सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2021 में दोनों सीमाओं पर अकेले वयस्कों को बड़ी संख्या में हिरासत में लिया गया था। अब दोनों सीमाओं पर हिरासत में लिए गए लोगों में से 16-18 फीसदी परिवार के साथ पाए गए।
इससे कई बार इस तरह के रास्तों से सीमा पार करने के दुखद नतीजे भी सामने आए हैं।
जनवरी 2022 में चार लोगों का एक भारतीय परिवार अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास करते समय कनाडा में अमेरिकी सीमा से महज़ 12 मीटर की दूरी पर ठंड से मारे गए। ये गुजरात से आए 11 लोगों के एक ग्रुप का हिस्सा थे।
वर्मोंट विश्वविद्यालय में इमिग्रेशन और शहरी मामलों पर अध्ययन करने वाले पाब्लो बोस कहते हैं कि भारतीय लोग बड़े आर्थिक मौक़ों और ‘अमेरिकी शहरों की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में जगह पाने की अधिक क्षमता’ के कारण बड़ी संख्या में अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसे लोग ख़ासतौर पर न्यूयॉर्क या बोस्टन जैसे बड़े शहरों में प्रवेश पाने की कोशिश करते हैं।
पाब्लो बोस ने बीबीसी को बताया, ‘मैं जो कुछ भी जानता हूँ और लोगों से जो बातचीत मैंने की है, उनसे पता चलता है कि ज़्यादातर भारतीय वर्मोंट या अपस्टेट न्यूयॉर्क जैसे ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में नहीं रह रहे हैं, बल्कि जितनी जल्दी हो सके शहरों की ओर जा रहे हैं।’
उनके मुताबिक़ वहाँ वे ज़्यादातर अनौपचारिक नौकरियाँ कर रहे हैं, जैसे घर और रेस्टोरेंट में काम करना।
अमेरिका में जल्द ही हालात और भी मुश्किल हो सकते हैं। अनुभवी इमिग्रेशन अधिकारी टॉम होमन जो जनवरी में ट्रंप के राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद देश की सीमाओं के प्रभारी होंगे।
उन्होंने कहा है कि कनाडा के साथ उत्तरी सीमा उनकी एक प्राथमिकता है क्योंकि इस क्षेत्र में अवैध प्रवास एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है।
अमेरिका में आगे क्या होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है।
पुरी कहती हैं, ‘यह देखना अभी बाक़ी है कि कनाडा अपनी सीमाओं से अमेरिका में आने वाले लोगों को रोकने के लिए ऐसी ही नीतियाँ लागू करेगा या नहीं। अगर ऐसा होता है, तो हम सीमा पर भारतीय नागरिकों की हिरासत में कमी की उम्मीद कर सकते हैं।’
जो भी हो हज़ारों हताश भारतीयों के अमेरिका में बेहतर जीवन की तलाश के सपने फीके पडऩे वाले नहीं हैं, भले ही आगे का रास्ता और अधिक खतरनाक हो। (bbc.com/hindi)
-दीपक मंडल
इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल जब बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत हासिल करने से रोकने में कामयाब रहे थे तो संभवत: सबसे ज़्यादा खुश कांग्रेस पार्टी हुई थी।
साल 2014 के लोकसभा चुनावों में 44 और और 2019 के लोकसभा चुनावों 52 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस को इस साल के लोकसभा चुनावों में 99 सीटों पर जीत मिलीं तो कई राजनीतिक विश्लेषकों और विशेषज्ञों ने इसे कांग्रेस की वापसी माना।
कांग्रेस ने संविधान, आरक्षण, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाकर लोकसभा चुनावों में बीजेपी और एनडीए को दबाव में लाने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल कर ली थी।
लेकिन लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस एक बार फिर से राज्यों के लिए हो रहे विधानसभा चुनावों में बुरी हार का सामना कर रही है। जहाँ कांग्रेस के सहयोगी दल जीत रहे हैं, वहाँ भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं दिखा है।
जून 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के चंद महीने बाद ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने थे और कांग्रेस के ‘जोश’ और ‘जज़्बे’ से ऐसा लग रहा था को वो ये चुनाव जीत लेगी।
राहुल गांधी संसद के बाहर और भीतर दोनों जगह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर पूरी तरह हमलावर थे।
लेकिन कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के साथ यही किस्सा अब राजनीतिक तौर पर देश के दूसरे बड़े अहम राज्य महाराष्ट्र में भी दोहराया गया।
झारखंड में पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुआई वाले गठबंधन में शामिल थी और वो 2019 में जीती 16 सीटों में एक भी सीट का इज़ाफा नहीं कर पाई।
इससे पहले, जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बुरी तरह नाकाम रही।
कांग्रेस 90 में से छह सीटें ही जीत पाईं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जूनियर पार्टनर बन कर किसी तरह अपनी नाक बचा पाई।
सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित दिख रही कांग्रेस इसके बाद एक भी राज्य का चुनाव क्यों नहीं जीत पाई। आखिर उसकी रणनीति में कहां खामी है और वो बार-बार कहां चूक रही है?
इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने कई राजनीतिक विश्लेषकों और पत्रकारों से बात की।
आइए समझते हैं हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना क्यों करना पड़ा।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) और अजित पवार की एनसीपी मिल कर महायुति गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही थीं।
बीजेपी 149, शिवसेना (शिंदे) 81 और अजित पवार की एनसीपी 59 सीटों पर लड़ रही थीं।
विपक्ष की ओर से महाविकास अघाड़ी यानी शिवसेना (उद्धव) 95, कांग्रेस 101 और एनसीपी (शरद पवार) 86 सीटों पर लड़ी थी।
महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर ज्यादातर एग्जि़ट पोल्स बीजेपी की अगुआई वाली महायुति की बढ़त तो दिखा रहे थे, लेकिन कुछ एग्जिट पोल्स महाविकास अघाड़ी को भी टक्कर देते हुए दिखा रहे थे।
लेकिन महायुति गठबंधन ने 288 में से 235 सीटों पर जीत हासिल की और उसका वोट शेयर रहा 49.6 फीसदी। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 35.3 फीसदी वोट मिले और इसे महज 49 सीटों से संतोष करना पड़ा है।
जो महाराष्ट्र एक दशक पहले तक कांग्रेस का गढ़ माना जाता था वहां उसे मात्र 16 सीटें मिली हैं।
आखिर महाराष्ट्र में कांग्रेस ने क्या गलती की कि उसका चुनावी प्रदर्शन इतना खराब रहा।
हमने ये सवाल पिछले कई सालों से कांग्रेस की राजनीति पर नजऱ रखने वाले विशेषज्ञ पत्रकार रशीद किदवई से पूछा।
उन्होंने कहा, ‘लोकतंत्र में पार्टियां चुनाव अपने कार्यकर्ताओं और संगठन के दमखम पर लड़तीं हैं। लेकिन अब चुनावी रणनीतिकारों की बन आई है। वो चुनाव स्ट्रैटेजी तय करते हैं, मुद्दे तय करते हैं और टिकट बांटने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। आजकल कांग्रेस में ये कल्चर ज्यादा हावी है। हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस चुनाव रणनीतिकारों पर निर्भर रही है। हरियाणा में भी यही हुआ था और महाराष्ट्र में भी यही दिखा।’
किदवई इसकी मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, ‘कांग्रेस हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी अपने चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुगोलू पर काफी ज्यादा निर्भर रही। कांग्रेस ने हरियाणा में हार से कोई सबक नहीं लिया, जहां गलत उम्मीदवारों को टिकट देने की शिकायतें की गई थीं।''
‘यहां तक कि एक मीटिंग में जब एक पार्टी नेता ने कानुगोलू के आकलन पर सवाल उठाया था तो राहुल गांधी ने उनका मज़ाक उड़ाया था। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े को भी टिकट बांटने की कवायद से अलग रखा गया।''
रशीद किदवई कहते हैं, ‘कांग्रेस की दूसरी गलती ये थी कि उसने सीएम चेहरा नहीं दिया। उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी का सीएम चेहरा था और कांग्रेस ने कभी इसका विरोध नहीं किया। राहुल गांधी हमेशा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ये कहते रहे कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को बलिदान देना सीखना चाहिए। दूसरी ओर राज्य में पार्टी के बड़े नेता आपस में लड़ते रहे।’
महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नेताओं में भी विरोधाभास दिखा।
किदवई कहते हैं, ‘कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और एनसीपी (शरद पवार) प्रमुख शरद पवार अलग-अलग सुर में बोलते रहे। जबकि,इस दौरान राहुल और खडग़े ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीजेपी के पास 'एक हैं सेफ़ हैं' जैसा नारा था जो इसकी स्ट्रैटेजी बता रहा था। लेकिन कांग्रेस अपनी रणनीति को समेटने वाला कोई मजबूत नारा सामने नहीं रख सकी।’
‘बीजेपी ने अपना चुनाव पूरी तरह पार्टी और आरएसएस के संगठन के बूते जीता। इस चुनाव में आरएसएस के चुनाव प्रबंधन ने अहम भूमिका निभाई। बीजेपी भी चुनावी रणनीतिकारों की मदद लेती है, लेकिन वो संगठन या पार्टी पर उसे हावी नहीं होने नहीं देती।’
उन्होंने कहा, ‘बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव पूरी तरह स्थानीय मुद्दों पर लड़ा। बीजेपी ने राज्य में हिंदू मतदाताओं के रुझान का ख्याल रखा। इसी के हिसाब से नारे गढ़े। लाडकी बहिन जैसी लाभार्थी योजना, आरक्षण के सवालों और महाराष्ट्र के किसानों के मुद्दों के इर्द-गिर्द अपनी रणनीति बनाई।’
विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस महाराष्ट्र से जुड़े स्थानीय मुद्दों को उठाने में नाकाम रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा चुनाव के नारे- संविधान बचाओ और जाति जनगणना के मुद्दे दोहराते रहे। यहां तक कि कांग्रेस राज्य में आरक्षण के सवाल पर मराठा और ओबीसी के अंतर्विरोध का भी फायदा नहीं उठा पाई।
यहां तक कि वो आरक्षण के अंदर आरक्षण के मुद्दे पर भी अपनी राय मतदाताओं के सामने नहीं रख सकी। सिफऱ् वो संविधान में आरक्षण को लेकर किए गए प्रावधानों को दोहराती रही।
इसी तरह की गलतियों की वजह से विदर्भ में कांग्रेस का करारी हार का सामना करना पड़ा जहां लोकसभा में कांग्रेस गठबंधन ने दस में से सात सीटें जीती थीं।
रशीद किदवई कहते हैं कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों के मुद्दे अलग-अलग होते हैं। लेकिन कांग्रेस महाराष्ट्र में मजबूत स्थानीय मुद्दे खड़े नहीं कर पाई। इसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा।
वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडणीस का मानना है कि कांग्रेस मतदाताओं में अपने वादों के प्रति विश्वास नहीं जगा सकी।
उन्होंंने बीबीसी हिंदी से कहा, ‘महाराष्ट्र सरकार ने ‘लाडकी बहिन’ योजना के जरिये पैसा पहुंचाकर ये सुनिश्चित किया कि उसके वादे में दम है। इस वजह से महिला वोटरों ने बड़ी तादाद में ‘महायुति’ के पक्ष में वोट दिया। कांग्रेस ने भी महिलाओं तक पैसे पहुंचाने का वादा किया। लेकिन सत्ता में ना होने की वजह से वो डिलीवरी के मामले में बीजेपी का मुक़ाबला नहीं कर सकती थी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस मतदाताओं में अपने वादों के प्रति भरोसा नहीं जगा सकी।’
अदिति फडणीस का ये भी कहना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति अलग होती है। कांग्रेस राज्यों के मुताबिक रणनीति नहीं तैयार नहीं कर पाई।
हरियाणा में भी कांग्रेस की रणनीति में ये कमजोरी दिखी और महाराष्ट्र में भी।
झारखंड
झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मिलकर 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। राज्य में 81 सीटें हैं। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीटें जीती हैं।
कांग्रेस ने सिर्फ 16 सीटें हासिल की हैं। गठबंधन में शामिल आरजेडी को चार और सीपीआई (माले) को दो सीटें मिली हैं।
यहां भी ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी गठबंधन के सत्ता में आने का दावा कर रहे थे। बीजेपी ने यहां असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनावी रणनीति को सिरे चढ़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी।
बीजेपी ने इस बार झारखंड में ‘बांग्लादेशी घुसपैठियों’ का भी मुद्दा उठाया लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन ने ‘आदिवासी बनाम बाहरी’ का मुद्दा चलाया और स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे पर झामुमो और ‘इंडिया’ गठबंधन की पार्टियों का साथ दिया। कांग्रेस के हिस्से 16 सीटें आईं।
कांग्रेस ने पिछली बार इतनी ही सीटें जीती थीं। आखिर वो अपनी सीटों में इजाफा क्यों नहीं कर पाई।
इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शरद गुप्ता कहते हैं, ‘कांग्रेस पूरे भारत में जो गलती कर रही है वही उसने झारखंड में भी की। मुद्दे पहचानने और उन्हें ज़मीन पर लाने में वो नाकाम रही। कांग्रेस की दूसरी बड़ी कमजोरी रही मजबूत केंद्रीय नेतृत्व का अभाव।’
वो कहते हैं, ‘मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा में क्षत्रपों की चली। उन्होंने अपनी मर्जी से टिकट बांटे। महाराष्ट्र की तरह झारखंड में कांग्रेस के नेता लड़ते रहे। पूरा फोकस चुनाव जीतने पर न होने से कांग्रेस को नुक़सान उठाना पड़ा।’
कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने राज्य में आदिवासी नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की इसका भी खमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा।
शरद गुप्ता भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं। वो कहते हैं, ‘झारखंड में कांग्रेस ने आदिवासी नेतृत्व बनाने की कभी कोशिश नहीं की। बीजेपी ने ये काम किया और उसने आदिवासी मुख्यमंत्री भी बनाए। अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी जैसे नेता बीजेपी ने ही दिए। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है।’
विश्लेषकों का कहना है कि ज्यादातर जगह कांग्रेस अब अपने मजबूती सहयोगियों की पीठ पर लदकर काम चला रही है। ये उसके भविष्य के लिए ठीक नहीं है।
शरद गुप्ता कहते हैं, ‘बिहार में आरजेडी, तमिलनाडु में डीएमके, जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस। हर जगह कांग्रेस अपने मजबूत सहयोगियों के बूते सीटें जीतने में कामयाब रही है। ओडिशा में कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका है। एक वक़्त में पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन अब वहां बीजेपी छाई हुई है। जबकि इन राज्यों की डेमोग्राफी कांग्रेस के पक्ष में हैं, लेकिन सरकारें बीजेपी की है।’
शरद गुप्ता कहते हैं, ‘कांग्रेस मुद्दे नहीं तय कर पा रही है। बीजेपी हर राज्य के हिसाब से मुद्दे तय करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सीट के हिसाब के मुद्दों के हिसाब से बोलते हैं। वहां के इतिहास, भूगोल, राजनीतिक परिस्थितियां सबको ध्यान में रख कर बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस इसके हिसाब से मुद्दे और रणनीति तय नहीं कर पाती।’
शरद गुप्ता कहते हैं कि मुद्दों के लिहाज से केंद्रीय नेतृत्व के थिंकटैंक में स्पष्टता न होना और इन्हें ज़मीन पर न उतार पाना कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी बन कर उभरी है। कांग्रेस इन कमजोरियों को दूर किए बिना राज्यों के चुनाव जीतने की उम्मीद छोड़ दे।
हरियाणा
2024 के अक्टूबर महीने में हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी ने यहां सत्ता विरोधी लहर, किसान और पहलवान आंदोलन के बावजूद जीत हासिल की और लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने में कामयाब रही।
हरियाणा चुनाव के नतीजों से पहले लगभग सभी एग्जिट पोल्स कांग्रेस को जीतते हुए दिखा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने इन्हें गलत साबित करते हुए बड़े आराम से बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए 48 सीटों पर जीत हासिल की ।
हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। बीजेपी को 39.9 प्रतिशत वोट मिले, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव (2019) की तुलना में 3.5 फीसदी ज़्यादा हैं। बीजेपी को पिछली बार से आठ सीटें ज़्यादा हासिल हुईं।
कांग्रेस सिर्फ 37 सीट ही जीत सकी। हालांकि ये पिछले विधानसभा चुनावों से छह ज़्यादा है।
सीटों के लिहाज से कांग्रेस कहां चूक गई। आखऱि उससे कहां गलती हुई?
इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री कहते हैं, ‘हरियाणा के चुनाव को कांग्रेस ने हल्के में लिया। जबकि ज़मीन पर जबरदस्त बीजेपी (सत्ता) विरोधी लहर थी। यहां कांग्रेस के हारने की दूसरी बड़ी वजह थी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई। इसका कुछ नुक़सान होता या नहीं, लेकिन इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने रेखांकित किया। उन्होंने पार्टी नेता सैलजा के कथित अपमान का जिक्र किया।’
हेमंत कहते हैं, ‘बीजेपी ने राज्य की ‘फॉल्टलाइन’ जाट बनाम गैर जाट के मुद्दे का भी बखूबी फ़ायदा उठाया। कांग्रेस में भी हुड्डा बनाम सैलजा की ‘लड़ाई’ का भी बीजेपी ने फ़ायदा उठाया। बीजेपी ने सीट दर सीट रणनीति तय की। उसने चुनाव जीतने लिए हर तरह के दांव खेले। जबकि कांग्रेस अति आत्मविश्वास की शिकार होकर रह गई।’
हेमंत अत्री कहते हैं कि कांग्रेस को जिस राज्य में अपनी अपनी स्थिति मजबूत दिखाई देती हो उसे वो हल्के में लेना शुरू कर देती है और फिर वहां वो रणनीतिक गलतियां शुरू कर देती है। चाहे वो अंदरूनी झगड़े का मामला हो या कैंडिडेट के चुनाव में गलतियां। कांग्रेस के अंदर बहुत जल्दी गुटबाजी शुरू हो जाती है।
वो कहते हैं, ‘बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को टिकट दे दिया वह पूरी पार्टी का उम्मीदवार होता है। लेकिन कांग्रेस में उम्मीदवार किसी एक गुट का कैंडिडेट होकर रह जाता है। फिर कांग्रेस का दूसरा गुट ही उसे हराने में लग जाता है। हरियाणा का चुनाव इसका उदाहरण था।’
वहीं, अदिति फडणीस कहती हैं कि हरियाणा में कांग्रेस अपने अंदरुनी झगड़ों की वजह से नुकसान में रही। कांग्रेस को पार्टी के अंदर इस प्रवृति रोकना होगा। वरना उसे आगे भी नुकसान उठाना पड़ सकता है।’ (bbc.com/hindi)
-अनघा पाठक
महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा से कुछ महीने पहले मुझे राज्य रानी एक्सप्रेस के जनरल कोच में यात्रा करने का मौका मिला था।
यह ट्रेन मुंबई को मराठवाड़ा से जोड़ती है, जो कि महाराष्ट्र का पिछड़ा इलाक़ा माना जाता है।
इसी कोच में महिलाओं के लिए एक छोटा सा हिस्सा आरक्षित है, जिसमें 12 सीटें दी गई हैं। मगर, यहां करीब 50 महिलाएं बैठी थीं।
ये सभी महिलाएं या तो अकेले या फिर अपनी दोस्त के साथ अपने-अपने शहर जा रही थीं। वे सभी महिलाएं गरीब और वंचित समुदाय से थीं।
लेकिन, वे अपने 15-20 घंटे इस छोटी जगह में बिताने के लिए तैयार थीं, क्योंकि उन्हें ‘मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना’ के लिए अपने दस्तावेज जमा करने थे।
योजना का कितना असर पड़ा?
चुनाव से ठीक पहले, महाराष्ट्र के महायुति गठबंधन की सरकार ने महिलाओं को इस योजना के ज़रिए हर महीने 1500 रुपये देने की घोषणा की थी। ये महिलाएं इसी योजना का फ़ायदा उठाने की उम्मीद में थीं।
कुछ महिलाओं को इस योजना से मिलने वाले पैसे से अपने बच्चे की स्कूल फीस भरनी थी, तो कुछ को दवाइयां खरीदनी थी। वहीं कुछ अपने लोन की किश्तें चुकाना चाहती थीं। उस समय किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस योजना का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन, आज इस बात का प्रमाण है कि इसकी बदौलत महायुति गठबंधन ने 230 सीटों के साथ चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है।
बीजेपी का वोट शेयर कैसे बढ़ा?
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का कहना है कि यह योजना विधानसभा चुनाव में गेमचेंजर साबित हुई।
कई एक्सपर्ट्स और विश्लेषकों का कहना है कि लाडली बहन और दूसरी योजनाओं ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की चुनाव जीतने में मदद की।
2024 के विधानसभा चुनाव में 2019 विधानसभा चुनाव के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या में लगभग 6 फ़ीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इन महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया।
कुमार केतकर एक वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और पूर्व सांसद हैं।
केतकर ने बीबीसी मराठी से कहा, ‘कई सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों ने 6-7 हजार वोटों से जीत हासिल की है।’
‘वहीं अगर आप करीब से देखें तो लगभग सभी सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या में भी 5-6 हजार की बढ़ोतरी हुई है। इन महिलाओं ने ही बीजेपी और उसके गठबंधन की जीत में अहम भूमिका निभाई है।’
क्या कहते हैं जानकार?
इससे यह सवाल उठता है कि क्या अब महिलाओं का एक अलग वोट बैंक बन गया है?
क्या अब महिलाएं उस सरकार को वोट देती हैं, जो उनके हित में काम करती है?
क्या वोटिंग, जो पहले जाति और धर्म से प्रभावित होती थी, वह अब महिला केंद्रित होती जा रही है?
अदिति नारायण पासवान दिल्ली यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।
वो इस बारे में कहती हैं, ‘हां यह बिल्कुल ठीक है कि वोटिंग पैटर्न अब जेंडर के आधार पर शिफ्ट हो गया है।’
‘हम महाराष्ट्र चुनाव में यह देख सकते हैं कि महिलाओं ने जाति और धर्म की राजनीति को पीछे छोडक़र उन पार्टियों या उम्मीदवारों को वोट दिया, जो उन्हें सीधे तौर पर फ़ायदा पहुंचा रहे थे।’
वह कहती हैं कि पिछले कुछ सालों में राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया है, जो कि 10 साल पहले नहीं हुआ करता था।
अदिति कहती हैं, ‘जब आप महिलाओं को कुछ सुविधाएं देते हैं, तो वे घर से निकलकर वोट डालने आती हैं। पहले महिलाओं को उनके पति बताते थे कि उन्हें किसे वोट करना है।’
‘हालांकि अब महिलाएं चुनावी राजनीति में सीधे तौर पर हिस्सा ले रही हैं। अब वे राजनीति में रुचि ले रही हैं। वे अब राजनीतिक दलों की बातों को ध्यान से सुन रही हैं और उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का आंकलन भी कर रही है।’
‘यह कोई नई बात नहीं है। 2019 के चुनाव में भी उज्ज्वला योजना ने हज़ारों महिलाओं की मदद की।’
योजना पर महिलाएं क्या सोचती हैं?
अगर महिला वोट बैंक बन जाता है, तो इसका भारत में चुनावी राजनीति के भविष्य पर क्या असर होगा?
प्रोफेसर अदिति पासवान बताती हैं, ‘कुछ लोग महिलाओं को वोट देने में मदद करने वाली योजनाओं की आलोचना करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कार्यक्रम महिलाओं को केवल वोट बैंक बनाता है। इससे उन्हें कभी भी समान प्रतिनिधित्व या समान अधिकार नहीं मिलते।’
‘हालांकि जब आप ज़मीनी स्तर पर जाकर गरीब महिलाओं से बात करते हैं, तो वे इन योजनाओं से मिलने वाली मदद से खुश होती हैं।’
‘उनका संघर्ष खुद को जिंदा रखना है। राजनीतिक दलों से मिलने वाला पैसा या दूसरी चीजें उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और परिवार में फैसला लेने में उनकी आवाज को मजबूत करती हैं। उनके लिए अभी यही बात सबसे जरूरी है।’
बल्कि, ये योजनाएं महिलाओं को चुनावी राजनीति में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करती हैं। वो मानती हैं कि इससे उनको भी प्रतिनिधित्व मिलता है।
विभूति पटेल मुंबई में एसएनडीटी वूमेंस यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की पूर्व प्रमुख हैं। वह भी इस बात से सहमत हैं।
विभूति कहती हैं, ‘आईएलओ और कई अन्य संगठनों द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि यात्रा में छूट देने और आर्थिक मदद देने से महिलाओं को काफी सहयोग मिलता है।’
‘महिलाओं को मिलने वाला पैसा शराब और सिगरेट पर ख़र्च नहीं होता। बल्कि, जब महिलाओं को पैसे मिलते हैं, तो वे इसका इस्तेमाल परिवार, खाने और बच्चों की पढ़ाई में करती हैं।’
योजना का एक पहलू ये भी है
सभी महिलाओं को लगता है कि उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए। उसको किसी से पैसे मांगने या अपने पति के सामने सफाई देने की जरूरत नहीं पडऩा चाहिए।
साधनाबाई ऐसी ही एक महिला थीं, जिनसे मेरी मुलाकात ट्रेन के जनरल डिब्बे में हुई थी।
उनके पति ने उन्हें छोडक़र दूसरी महिला से शादी कर ली थी। उनकी 18 साल की बेटी ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था।
वह नौकरानी का काम करके जो पैसे कमाती थी, वे उनके लिए काफी नहीं थे।
इसलिए, अपने दामाद पर निर्भर रहने के बजाय वह इस उम्मीद में थी कि उनको लाडक़ी बहिन योजना के पैसे मिल जाए। इसलिए, वह ट्रेन में खड़े होकर 15 घंटे का सफर करने को तैयार थीं।
अर्थशास्त्री अभय तिलक ऐसी योजनाओं का आंकलन करते हुए कहते हैं, ‘महिलाओं की एक बड़ी संख्या ऐसी है, जिसके पास पैसे कमाने का कोई ज़रिया नहीं है।’
‘परिवार में उनके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। लेकिन ऐसी योजनाओं से इन महिलाओं को कुछ पैसे मिल रहे हैं और उनके परिवारों में उनकी स्थिति सुधर रही है।’
हालांकि, उन्हें एक चिंता है।
अभय कहते हैं, ‘व्यक्तिगत स्तर पर इस योजना से लोग तो खुश हैं। लेकिन, माइक्रो लेवल पर लाडक़ी बहिन जैसी योजना का महंगाई पर असर पड़ेगा। और मैं यह सोचता रहता हूं कि आर्थिक तौर पर यह टिकाऊ नहीं रहने वाला है।’
कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन योजनाओं से किसी राजनीतिक पार्टी को लंबे समय तक सत्ता में बने रहने में मदद नहीं मिल सकती।
मतदाता के मन में क्या?
नवेंदु पटना के वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने बिहार की राजनीति पर बहुत बारीकी से काम किया है।
बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं लागू की हैं। इससे मिले नतीजों को नवेंदु ने देखा है।
लेकिन, योजनाओं से बनने वाले वोट बैंक के बारे में बात करते हुए वह कहते हैं, ‘जो पार्टी या उम्मीदवार सबसे ज़्यादा ऑफर करता है, और लोग उसको पसंद करते हैं तो उसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं।’
‘लेकिन, अगर ऐसा वोट बैंक बन भी जाता है, तो यह स्थिर नहीं होगा। क्योंकि, लोगों का वोट दूसरी जगह पर शिफ्ट होता रहेगा।’
लेकिन, अब लोग विचारधारा की जगह इस आधार पर वोट कर रहे हैं कि किस राजनेता या राजनीतिक दल से उन्हें व्यक्तिगत तौर पर क्या फायदा मिल रहा है।
ऐसा केवल महिलाओं के साथ ही नहीं, बल्कि सभी के साथ हो रहा है।
बीबीसी मराठी से बात करते हुए कुमार केतकर कहते हैं, ‘इन दिनों एक चलन तेज़ी से बढ़ रहा है, जो व्यक्ति केंद्रित है। मतलब यह कि लोग अब केवल नागरिक या मतदाता नहीं रह गए हैं।’
‘अब वह एक व्यक्ति या स्वतंत्र उपभोक्ता बन चुके हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप उनसे जुड़ा जो भी फ़ैसला लें, तो उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखें।’
इस तरह के वादे और कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के मामले में उनकी व्यक्तिगत चुनौतियों को सामने लाती हैं।
हालांकि, एक पहलू यह भी है कि अगर महिलाओं को अलग-अलग सरकारों द्वारा वित्तीय मदद दे दी जाती है, तो उनके सामाजिक न्याय और समानता का क्या होगा? साथ ही उनकी राजनीतिक भागीदारी का सवाल भी हमारे सामने होगा।
डॉ. गोपाल गुरु दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग के रिटायर्ड प्रोफेसर और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं।
वह कहते हैं, ‘कल्याणकारी राज्य वह होता है, जहां सरकार राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक समानता लाने के लिए कदम उठाती है।’
‘लेकिन, हमें बिना किसी कारण लोगों को पैसा देने के बारे में सोचना होगा। जब सरकार कोई वित्तीय मदद देती है, तो उसके पीछे कोई उचित कारण होना चाहिए।’
‘सरकार किसी व्यक्ति को पैसा क्यों दे रही है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। श्रमिक के आत्मसम्मान के बारे में भी सोचा जाना चाहिए।’
‘पैसा देने की जगह सरकार को लोगों के आर्थिक हालात को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। मनरेगा इसका एक अच्छा उदाहरण है।’
महिला मतदाताओं को लुभाने की पिछली कोशिशें
मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव साल 2023 में हुए थे। वहां भी ‘लाडली बहन’ के नाम से ऐसी ही योजना की शुरुआत की गई।
इस योजना के तहत सरकार द्वारा 23 से 60 साल की आयु वाली गरीब महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीने देने की घोषणा की गई।
सरकार ने दावा किया कि इस योजना से 1।25 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को फायदा पहुंचा। इसी योजना ने मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत दिलाने में मदद की।
लेकिन, बीजेपी ऐसी योजनाओं को लागू करने वाली अकेली पार्टी नहीं है। इससे पहले भी कई राज्यों की सरकारों ने महिलाओं को अपनी तरफ खींचने और अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश की है।
बिहार इसका एक उदाहरण है।
नीतीश कुमार ने 2007 के आसपास स्कूल की छात्राओं को साइकिल देने वाली योजना की शुरुआत की थी। जिसमें आठवीं पास करने वाली हर लडक़ी को साइकिल खरीदने के लिए पैसे दिए जाते थे।
उस समय नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे संजय झा ने कहा था, ‘साल 2006 में मुख्यमंत्री साइकिल योजना को लागू किया गया, जिसके कारण बिहार में लड़कियों की शिक्षा में बड़ा बदलाव आया।’
‘आंकड़ों से पता चलता है कि जहां साल 2007 में 10वीं कक्षा में पढऩे वाली लड़कियों की संख्या 1।87 लाख थी। वह साल 2022 में बढक़र 8।37 लाख हो गई।’ कई लोगों का मानना है कि साइकिल ने बिहार में हज़ारों लड़कियों के लिए शिक्षा के दरवाजों को खोला है।
वरिष्ठ पत्रकार नवेंदु कहते हैं, ‘बिहार में आज भी शिक्षा के हालात अच्छे नहीं है। गांवों में कोई स्कूल या कॉलेज ही नहीं है। लेकिन, तब के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़ाब थे।’ ‘जब लड़कियों को सरकार की तरफ से साइकिल मिली, तो उन्हें सुरक्षित और तेज़ परिवहन का साधन मिला। इससे उन्हें सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर नहीं रहना पड़ा।’
‘लड़कियां अपने गांव से बाहर स्कूल, कॉलेज जाने लगी, जिससे एक सामाजिक बदलाव आया।’
‘इस कारण लड़कियों की माताओं ने नीतीश कुमार को वोट दिया, क्योंकि वे अपनी बेटियों के लिए अच्छी जिंदगी चाहती थी।’
यह महिलाओं को सीधे फायदा पहुंचाने वाली सबसे पहली कोशिशों में से एक थी। जिसको लेकर नवेंदु कहते हैं कि यह कोशिश पूरी तरह से सफल हुई।
इन नेताओं के साथ महिला वोटर्स
महिलाओं के लिए नीतीश सरकार का दूसरा अहम फैसला शराबबंदी का था।
नवेंदु कहते हैं, ‘शराबबंदी से कई चीज़ें जुड़ी हुई थी। घर के मर्द शराब पर सारा पैसा खर्च कर देते थे, जिसके कारण महिलाओं को गरीबी का सामना करना पड़ता था।’ ‘साथ ही महिलाओं को घरेलू हिंसा और यौन उत्पीडऩ जैसी समस्याओं को झेलना पड़ता था।’
‘लेकिन, नीतीश सरकार के शराबबंदी वाले फैसले ने महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने में मदद की, जिसके नतीजे आज भी दिख रहे हैं।’
इसलिए, नीतीश कुमार को वोट देने वाली महिलाएं उनके मुश्किल समय में उनके साथ बनी हुई हैं।
इसी कारण से नीतीश सरकार ने अपने शराबबंदी के फ़ैसले को बरकरार रखा है, भले ही उनकी राजनीतिक सहयोगी बीजेपी इस फैसले के ख़िलाफ़ हों।
तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता भी महिलाओं को मदद करने वाली योजनाओं के लिए जानी जाती थीं। इसी कारण से हजारों महिलाएं उनका समर्थन करती थी और जयललिता के लिए वोट बैंक बनी हुई थीं।
इसके अलावा, पिछले साल कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए कई बड़े वादे किए थे। जिसमें से एक घोषणा सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की थी।
वहीं, दूसरी योजनाओं में महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह देने के साथ-साथ रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की घोषणा भी की गई थी।
जब कांग्रेस की सरकार बनी, तब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपनी मुफ्त बस यात्रा और रसोई गैस सिलेंडर पर 300 रुपये की छूट देने का वादा पूरा किया।
सीतालक्ष्मी हैदराबाद में रहती हैं। वह खुद मुफ्त बस यात्रा योजना का फायदा उठाती हैं।
वह कहती हैं, ‘मुझे अब पूरे राज्य में कही भी जाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अपना आधार कार्ड दिखाकर कहीं भी जा सकती हूं। इसने हज़ारों महिलाओं को घर से बाहर निकलने का मौका दिया है।’
वह यह भी मानती हैं कि मुफ्त सार्वजनिक परिवहन ने गरीब महिलाओं की बहुत मदद की है।
सीतालक्ष्मी कहती हैं, ‘अब अगर किसी महिला को उसके पति ने पीटा है और घर से बाहर निकाल दिया है, तो वह बिना किसी पैसे के अपनी मां के घर वापस जा सकती है।’
‘इसलिए हमें ऐसी सरकार को वोट क्यों नहीं देना चाहिए, जो हमें ऐसी योजनाएं मुहैया कराती है।’
प्रोफ़ेसर अदिति पासवान को इसलिए लगता है कि आने वाले समय में महिला मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए राजनीतिक पार्टियां ऐसी और योजनाएं लाएंगी।
वह कहती हैं, ‘यह सच है कि ऐसी योजनाओं से सीधा फायदा मिलेगा, साथ ही समाज में राजनीतिक समानता भी आएगी। इससे पुरुषों और महिलाओं का वोटिंग पैटर्न भी बदलेगा।’
‘हालांकि, इन योजनाओं के कुछ नुकसान भी है, जो महिलाओं को वोट बैंक बना रहे हैं।’
‘लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इन योजनाओं से महिलाओं के हालात सुधरने शुरू हुए हैं। जैसे-जैसे महिला मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ेगा, राजनीति में उनकी हिस्सेदारी भी बढ़ेगी।’ (bbc.com/hindi)
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के चेयरमैन इमरान ख़ान के समर्थक सडक़ों पर हैं।
समर्थक पुलिस और प्रशासन से भिड़ रहे हैं ताकि उनके नेता की जेल से रिहाई हो सके। लेकिन इन सबके बीच पाकिस्तान की राजनीति में सऊदी अरब के बारे में एक बयान चर्चा में है।
पिछले हफ़्ते गुरुवार को इमरान ख़ान की पत्नी बुशरा बीबी ने एक वीडियो संदेश में कहा था कि जब इमरान ख़ान मदीना से वापस आए थे, तब पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख क़मर जावेद बाजवा के पास फोन आया था कि आप किसे लेकर आ गए हो।
सितंबर 2019 में इमरान ख़ान अपनी पत्नी बुशरा बीबी के साथ उमरा के लिए मदीना गए थे।
दरअसल बुशरा बीबी इमरान ख़ान से जेल में मिलने गई थीं और इस मुलाक़ात के बाद ही उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया था।
लगभग आधे घंटे के इस वीडियो संदेश में बुशरा बीवी के 50 सेकेंड के हिस्से पर ख़ासा विवाद हो रहा है। इसे लेकर बुशरा बीबी के खिलाफ कई मुक़दमे भी दर्ज हो गए हैं।
बुशरा बीबी की जिस बात पर विवाद हो रहा है, उसमें उन्होंने कहा है, ‘इमरान ख़ान के पीछे जो सारी ताक़तें खड़ी हो गई हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, ये आपसे किसी ने नहीं बताई।’
उन्होंने बताया, ''मैं आज ये बात आप सबसे बताती हूँ। ख़ान जब सबसे पहले मदीना शरीफ़ नंगे पाँव गए थे और वहाँ से वापस आए, तो फौरन ही जनरल बाजवा को फोन आने शुरू हो गए थे।’
उनके मुताबिक़ बाजवा से फोन पर पूछा गया, ''ये तुम किसे उठाकर लाए हो। हम इस मुल्क से शरीअत के निजाम ख़त्म करने में लगे हैं और तुम शरीअत के ठेकेदारों को लाए हो। हमें ये नहीं चाहिए।''
बुशरा बीबी ने उस वीडियो में कहा, ‘आप ये यक़ीन मानिए तब से ख़ान, उसकी बेगम को निशाने पर लिया जाने लगा और ख़ान को यहूदियों का एजेंट कहना शुरू कर दिया गया। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि ख़ान ने इसे कभी पब्लिक में नहीं बताया। अगर ये बात ग़लत है तो फिर जनरल बाजवा और उसकी फैमिली से पूछिए। बाजवा और उसकी फैमिली ने ही ये बात किसी को बताई थी, जो बाद में ख़ान तक पहुँची थी। ख़ान को नंगे पाँव मदीना जाने के लिए सज़ा दी जा रही है।’
बुशरा बीबी की इस बात पर पाकिस्तान में हंगामा मच गया है।
बुशरा बीबी के खिलाफ पाकिस्तान में इस बयान के कारण कई नए मुक़दमे दर्ज हो गए हैं।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा है कि सऊदी अरब के बारे में ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त से बाहर है।
शहबाज़ शरीफ़ ने बीते शुक्रवार को इस्लामाबाद में कहा था, ''सऊदी अरब ने हर मोर्चे पर बिना शर्त पाकिस्तान का समर्थन किया है। सऊदी अरब ने भाई की तरह मदद की है। बदकिस्मती से कल जो बयान आया है, वो पाकिस्तान से दुश्मनी निकालने की तरह है। सऊदी जैसे दोस्त और भाई के ख़िलाफ़ ज़हर उगला जा रहा है। हमें मुल्क के दुश्मनों का डटकर मुक़ाबला करना होगा। हम किसी को भी सऊदी अरब से रिश्ते बिगाडऩे की इजाज़त नहीं दे सकते हैं।’
बुशरा बीबी के बयान पर पाकिस्तान में काफ़ी बहस हो रही है।
भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल एबीएन से बातचीत में कहा, ‘सबसे पहले तो बुशरा बीबी को यह बात नहीं कहनी चाहिए थी कि वहाँ से फोन आया। हालांकि हुकूमत की तब्दीली में सऊदी का हाथ नहीं था। 2018 में इमरान ख़ान ने पहला दौरा सऊदी अरब का किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते तकऱीबन आठ दौरे सऊदी अरब के किए। इनमें से कुछ ओआईसी की मीटिंग भी शामिल थीं।’
बुशरा बीबी ने ऐसा क्यों कहा?
अब्दुल बासित ने कहा, ‘सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी फऱवरी 2019 में पाकिस्तान आए थे। उसके बाद भी इमरान ख़ान सऊदी अरब गए। एमबीएस और इमरान के बीच अच्छे संबंध रहे थे।’
बासित कहते हैं कि एक मौक़ा जरूर आया, जब सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान से नाराज़ हुए थे।
बासित ने टीवी कार्यक्रम के दौरान कहा, ''वो मौक़ा था, जब भारत ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया। हमें उम्मीद थी कि शायद सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। लेकिन वो नहीं हुआ। इसे लेकर हमारी फ्रस्ट्रेशन थी। तब मलेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति महातिर मोहम्मद ने इस्लामिक दुनिया को ओआईसी अलग एकजुट करने की कोशिश की और इस मुहिम में इमरान ख़ान ने भी दिलचस्पी दिखाई थी। यह सऊदी और यूएई को रास यह नहीं आया था।''
अब्दुल बासित के मुताबिक़ सऊदी अरब की नाराजग़ी के बाद इमरान ख़ान को अपने क़दम पीछे खींचने पड़े थे।
बासित ने बताया कि सऊदी अरब का पाकिस्तान के सियासी मामलों में प्रभाव रहा है। वो चाहे ज़ुल्फक़िार अली भुट्टों को फांसी लगाने से बचाने का मामला हो या फिर नवाज़ शरीफ़ के निर्वासन में उसकी भूमिका हो।
हालांकि पूर्व डिप्लोमेट अब्दुल बासित को लगता है कि शहबाज़ शरीफ़ को इस पर बयान नहीं देना चाहिए था और सऊदी अरब को घरेलू सियासत में नहीं लाना चाहिए था।
बासित ने कहा, ‘यह हमारे मुल्क के हितों के बिल्कुल खिलाफ है।’
पाकिस्तान की जानी-मानी रक्षा विश्लेषक डॉ आयशा सिद्दीक़ा ने पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल नया दौर के रज़ा रुमी से कहा, ''संभव है कि सऊदी अरब ने बाजवा से कहा हो कि किसे साथ लाए हो। लेकिन इसमें मिलावट की गई है वो ठीक नहीं है। इमरान ख़ान ने सऊदी के क्राउन प्रिंस के लिए गाड़ी चलाई थी।’
आयशा सिद्दीक़ा ने चैनल को बताया, ‘इमरान ख़ान जब वहाँ गए तो उन्होंने सऊदी अरब के बादशाह के लिए प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था। बादशाह खड़े थे और वो आगे निकल गए थे। फिर उन्हें रोका गया था। यूएन में भी ईरान और सऊदी अरब की बात करने लगे थे। लेकिन सऊदी ने इन्हें हटा दिया, ये बात ठीक नहीं है।’
बुशरा का दांव उल्टा पड़ेगा?
आयशा सिद्दीक़ा को नहीं लगता कि इससे सऊदी अरब से संबंध खऱाब होंगे लेकिन फौज की सख़्ती पीटीआई के ख़िलाफ़ बढ़ जाएगी।
उन्होंने कहा, ‘बुशरा बीबी ने दरअसल ये बात सऊदी अरब से संबंध खऱाब करने के लिए ही की है। सऊदी अरब में पाकिस्तान के लाखों लोग काम करते हैं और इनमें ज़्यादातर इमरान ख़ान के समर्थक हैं। वहाँ इमरान ख़ान के हक़ में नारे लगाए जाएँगे, तो सऊदी बहुत सख़्त कार्रवाई करेगा।’
आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, ''अगर इमरान ख़ान फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो किस मुँह से सऊदी अरब मांगने जाएंगे। ये सवाल तो उन्हें ख़ुद से करना चाहिए। मुझे लगता है कि हर हाल में इमरान ख़ान ने अपनी बेगम से बयान दिलवाकर अपना नुक़सान कराया है।’
‘अब तो सऊदी अरब इमरान ख़ान को बाहर लाने में भी मदद नहीं कर सकता है। इन सबके बावजूद बुशरा बीबी ने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब है कि बुशरा बीबी ने ऐसा ख़ान साहब के कहने पर किया है। इमरान ख़ान चाहते हैं कि सऊदी अरब से पाकिस्तान के ताल्लुकात खऱाब हो जाएं और आर्थिक मदद ना मिले ताकि मौजूदा सरकार के प्रति लोगों का ग़ुस्सा बढ़े। ये कहना कि सऊदी अरब शरीअत से बाहर हो गया है बिल्कुल झूठ है। सऊदी अरब अपने हिसाब से शरीअत पर ही चल रहा है।’
पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल जीओ न्यूज़ से पूरे विवाद पर जनरल (रिटायर्ड) क़मर जावेद बाजवा ने कहा कि बुशरा बीबी के आरोप बेबुनियाद हैं।
जनरल (रिटायर्ड) बाजवा ने कहा, ‘बेबुनियाद आरोपों से सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करना चाहिए। अब तक के इतिहास में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बिना शर्त समर्थन किया है, वो चाहे जिसकी भी सरकार रही हो। बुशरा बीबी के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं।’ (bbc.com/hindi)
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसराइल और ईरान समर्थित हथियारबंद समूह हिज़्बुल्लाह के बीच एक युद्धविराम समझौते की घोषणा की है।
इसके साथ ही इसराइल और हिज्बुल्लाह के बीच पिछले 13 महीनों से चल रही लड़ाई थम जाएगी।
अमेरिका और फ्ऱांस के संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस समझौते से लेबनान में जारी जंग रुकेगी और ‘इसराइल पर भी हिज़्बुल्लाह और अन्य आतंकवादी संगठनों के हमले का ख़तरा’ टल जाएगा।
युद्धविराम के बारे में हमें क्या पता है?
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने पत्रकारों से कहा कि इस समझौते को स्थायी युद्धविराम के रूप में लाया गया है। युद्धविराम की शर्तों के मुताबिक़ 60 दिनों में हिज़्बुल्लाह अपने लड़ाकों और हथियारों को ब्लू लाइन के बीच से हटा लेगा।
समझौते की शर्तों के मुताबिक इन इलाक़ों में हिज़्बुल्लाह के लड़ाकों की जगह लेबनान के सैनिक होंगे। लेबनान के सैनिक इसे सुनिश्चित करेंगे कि इन इलाक़ों से हिज्बुल्लाह के इन्फ्ऱास्ट्रक्चर और हथियारों को हटाया जाए और इसे फिर से न बनने दिया जाए।
बाइडन ने कहा कि इन 60 दिनों में इसराइल धीरे-धीरे अपने सैनिकों और नागरिकों को वापस बुलाएगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आम लोग सरहद से लगे इलाक़ों में अपने घर लौट सकें।
पाँच हज़ार लेबनानी सैनिक हिज़्बुल्लाह की जगह लेंगे
अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक़ लेबनान की सेना दक्षिण में पाँच हज़ार सैनिकों को तैनात करेगी।
हालांकि सवाल अब भी बाक़ी हैं कि युद्धविराम लागू करने में इनकी क्या भूमिका होगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या ये हिज़्बुल्लाह से लड़ेंगे?
लेबनान के लोग धार्मिक समूहों में बँटे हुए हैं और इस बात की गहरी आशंका रहती है कि कहीं आपस में ना उलझ जाएं।
लेबनान की सेना ने कहा है कि उसके पास कोई संसाधन नहीं है। न पैसे हैं, न लोग और न ही सैन्य उपकरण। ऐसे में इस समझौते की शर्तों को पूरा करना आसान नहीं है।
हालांकि कहा जा रहा है कि लेबनान के वैश्विक सहयोगी आर्थिक मदद कर सकते हैं। पश्चिम के देशों के कई अधिकारियों ने कहा कि हिज़्बुल्लाह अब कमज़ोर हो गया है और लेबनान की सरकार के लिए यह मौक़ा है कि अपने इलाक़ों को नियंत्रण में ले।
युद्धविराम की निगरानी कौन करेगा?
यह समझौता लगभग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 जैसा है, जिससे 2006 में इसराइल और हिज़्बुल्लाह के बीच युद्ध का अंत हुआ था।
प्रस्ताव 1701 में था कि लिटानी नदी के दक्षिणी इलाक़े में लेबनानी सैनिकों और यूएन के शांति सैनिकों के अलावा कोई और दूसरा हथियारबंद समूह नहीं रह सकता है। लेकिन दोनों पक्ष समझौते के उल्लंघन का दावा करते थे।
इसराइल का कहना था कि हिज़्बुल्लाह को इस इलाक़े में व्यापक पैमाने पर निर्माण की अनुमति दी गई थी। वहीं लेबनान का कहना था कि इसराइल समझौते का उल्लंघन करता था।
अमेरिका के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इस बार अमेरिका और फ्रांस मौजूदा त्रिपक्षीय व्यवस्था में शामिल होंगे। इस त्रिपक्षीय तंत्र में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल, लेबनान और इसराइल हैं।
इन्हीं के ज़िम्मे युद्धविराम की निगरानी की ज़िम्मेदारी है।
इस इलाक़े में अमेरिकी सैनिक नहीं होंगे लेकिन लेबनानी सेना की मदद के लिए सैन्य सहयोग रहेगा।
ऐसा अतीत में भी किया गया है। फ्ऱांस भी लेबनान की सेना को मदद देगा।
बाइडन ने इसराइली चिंता का ज़िक्र करते हुए कहा, ‘हिज़्बुल्लाह के आतंकवादियों को दक्षिणी लेबनान में किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।’
इसराइल ने क्या कहा?
इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा ‘अमेरिका की सोच’ के साथ इसराइल लेबनान में ‘सैन्य कार्रवाई की पूरी आज़ादी’ को जारी रखेगा।
इसराइली प्रधानमंत्री ने कहा, ‘अगर हिज़्बुल्लाह ने समझौते का उल्लंघन किया और हथियार उठाए तो हम हमला करेंगे। अगर सरहद के पास आतंकवादी आधारभूत ढाँचा फिर से बनाया जाएगा तो हम हमला करेंगे। अगर रॉकेट लॉन्च किए गए, टनल बनाए गए और ट्रकों से रॉकेट लाए गए तो हम हमला करेंगे।’
बाइडन ने बिन्यामिन नेतन्याहू का समर्थन करते हुए कहा, ‘अगर हिज़्बुल्लाह या किसी ने समझौते को उल्लंघन किया और इसराइल के लिए ख़तरा पैदा किया तो उसके पास अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक़ आत्मरक्षा का अधिकार होगा।’
लेकिन बाइडन ने ये भी कहा है कि समझौता लेबनान की संप्रभुता को बरकरार रखता है। इसराइल के हमले का अधिकार इस समझौते का हिस्सा नहीं है क्योंकि लेबनान ने इसका विरोध किया था।
कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर अमेरिका बाद में एक पत्र जारी कर इसराइल के हमले का अधिकार का समर्थन करेगा। (bbc.com/hindi)
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से ही कहा जा रहा था कि कनाडा के लिए वो मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं।
सोमवार को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह कनाडा से अमेरिका आने वाले हर उत्पाद पर 25 फ़ीसदी टैरिफ लगाएंगे।
ट्रंप ने कनाडा के अलावा एक और पड़ोसी देश मेक्सिको के भी सभी उत्पादों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि वो चीन के सभी उत्पादों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे।
ट्रंप ने कहा कि कनाडा और मेक्सिको के ख़िलाफ़ यह टैरिफ प्रवासियों और अवैध ड्रग्स को रोकने के लिए जरूरी है।
ट्रंप ने ट्रूथ सोशल नेटवर्क पर एक पोस्ट में लिखा है कि 20 जनवरी को ऑफिस संभालते ही कनाडा, मेक्सिको और चीन के खिलाफ टैरिफ लगाने के लिए एक ‘कार्यकारी आदेश’ पर हस्ताक्षर करेंगे।
ट्रंप ने कहा, ‘सभी को पता है कि कनाडा और मेक्सिको से हज़ारों लोग अमेरिका में घुस रहे हैं। ये अपने साथ ड्रग्स ला रहे हैं और कई अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। जिस स्तर पर ये सब हो रहा है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ।’
ट्रंप बनाम ट्रूडो
कनाडा और अमेरिका के बीच दुनिया का सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है और दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंध एक ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का है।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप की जीत के तत्काल बाद ही बधाई दी थी लेकिन दोनों नेताओं के संबंधों में पर्याप्त तनाव रहा है।
अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति कमान संभालने के बाद पारंपरिक रूप से पहला विदेशी दौरा कनाडा या मेक्सिको का करता था लेकिन ट्रंप ने 2017 में पहला विदेशी दौरा सऊदी अरब का किया था। यानी ट्रंप ने आते ही संदेश दे दिया था।
जस्टिन ट्रूडो पर ट्रंप व्यक्तिगत हमले भी करते रहे हैं। ट्रूडो को ट्रंप ने ‘घोर-वामपंथी पागल’ कहा था।
कनाडा की आर्थिक स्थिति पहले से ही चिंताजनक है और ट्रंप के टैरिफ से वहाँ की अर्थव्यवस्था के मंदी में जाने की आशंका बढ़ जाएगी।
कनाडा का 75 प्रतिशत निर्यात अमेरिका में होता है। ऐसे में 25 प्रतिशत का टैरिफ कनाडा को भारी पड़ सकता है।ट्रूडो के लिए ये मुश्किलें तब खड़ी हो रही हैं, जब कनाडा में चुनाव सिर पर है। कई चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में बताया जा रहा है कि ट्रूडो चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी से हार सकते हैं।
पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में रहना काफी महंगा हुआ है। दूसरी तरफ कनाडा पहले से ही चीन और भारत से उलझा हुआ है। ऐसे में कनाडा के लिए अपना व्यापार अमेरिका से बाहर ले जाना भी आसान नहीं है।
मोदी सरकार जस्टिन ट्रूडो पर कनाडा में रह रहे खालिस्तानी अलगाववादियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाती रही है।
दूसरी तरफ जस्टिन ट्रूडो सरकार कनाडा में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा रही है। इस मामले में बाइडन प्रशासन ट्रूडो के साथ था।
अब कहा जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानी अलगाववादियों के मामले में शायद कोई समर्थन न मिले।
ट्रंप-ट्रूडो और मोदी
जिस तरह से ट्रंप और ट्रूडो के व्यक्तिगत संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, उसी तरह मोदी और ट्रूडो के भी आपसी संबंधों में गर्मजोशी नहीं है।
मोदी मई 2014 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने और जस्टिन ट्रूडो अक्तूबर 2015 में पहली बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने।
2019 में भी नरेंद्र मोदी दूसरे कार्यकाल के लिए चुनकर आए और ट्रूडो को भी अक्टूबर 2019 में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया।
ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा ख़ुद को उदारवादी लोकतांत्रिक बताती है और पीएम मोदी की बीजेपी की पहचान हिन्दुत्व और दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी के रूप में है।
प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने अप्रैल 2015 में कनाडा का दो दिवसीय दौरा किया था। उस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री कन्जर्वेटिव पार्टी के स्टीफन हार्पर थे।
2010 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी-20 समिट में शामिल होने कनाडा गए थे। लेकिन समिट से इतर किसी भारतीय प्रधानमंत्री का कनाडा जाना 42 साल बाद तब हो पाया, जब पीएम मोदी कनाडा के दौरे पर 2015 में गए।
जस्टिन ट्रूडो जब से पीएम बने हैं, तब से नरेंद्र मोदी कनाडा नहीं गए हैं।
कनाडा दुनिया का चौथा बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक है लेकिन ट्रंप का टैरिफ ऊर्जा से हासिल होने वाले राजस्व पर भी भारी चोट करेगा। दूसरी तरफ़ ट्रंप अमेरिका में घरेलू ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं।
2022 में ट्रूडो ने अमेरिका से आने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए वैक्सीन लगाना अनिवार्य कर दिया था। इसके लिए ट्रंप ने ट्रूडो को ‘घोर-वामपंथी पागल’ कहा था।
जून 2018 में ट्रंप कनाडा के क्यूबेक में आयोजित जी-7 समिट के बीच से ही निकल गए थे और उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को ‘घोर बेईमान और कमजोर’ नेता कहा था।
जस्टिन ट्रूडो को पहले से ही थी आशंका
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पर कनाडा में सबकी नजरें टिकी थीं। ट्रंप की जीत के बाद एक संदेश गया कि कनाडा की चुनौतियां बढऩे वाली हैं।
रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप की जीत के बाद कनाडा की वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा था, ''कनाडा में बड़ी संख्या में लोग अमेरिकी चुनाव को लेकर तनाव में थे। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अमेरिका से हमारा गहरा संबंध है और ट्रंप के साथ भी हमारे मज़बूत संबंध हैं।’ इसी साल जनवरी में ट्रूडो ने कहा था कि ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो कनाडा के लोगों की जिंदगी मुश्किल होगी और यह एक कदम पीछे जाने की तरह होगा।
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, वित्तीय मामलों के थिंक टैंक डिजार्डियंस के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि ट्रंप की नीतियों के कारण 2028 के अंत तक कनाडा की जीडीपी में 1.7 फीसदी तक गिरावट आ सकती है।
ट्रंप 2017 में पहली बार जब राष्ट्रपति बने थे, तब उन्होंने उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की बात कही थी। अमेरिका का यह समझौता मेक्सिको और कनाडा के साथ है।
ट्रंप की शिकायत रही है कि इस समझौते से अमेरिका को नुकसान हो रहा है और बाक़ी दोनों देशों को फायदा हो रहा है।
इस समझौते को लेकर कनाडा और अमेरिका 18 महीनों तक तनाव भरे माहौल बातचीत हुई थी लेकिन बेनतीजा रही थी और दोनों देशों ने एक दूसरे के उत्पादों पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था।
इसके बाद यह समझौता यूएस-मेक्सिको-कनाडा डील के रूप में सामने आई थी। लेकिन ट्रंप ने 11 अक्तूबर को इसकी समीक्षा की भी बात कही थी।
समाचार एजेंसी रॉर्यटर्स के अनुसार, इसी साल जनवरी में ट्रूडो ने एक मीटिंग में अपनी लिबरल्स पार्टी के सीनियर नेताओं से कहा था कि कनाडा के लिए ट्रंप का दूसरा कार्यकाल पहले कार्यकाल से ज़्यादा चुनौती पूर्ण होगा। यह बात रॉयटर्स से एक सूत्र ने बताई थी, जो उस मीटिंग में ख़ुद भी मौजूद था। (bbc.com/hindi)
-डॉ. आर.के. पालीवाल
देश की जनता ने महाराष्ट्र में पिछले पांच साल में राजनीति को कई गड्ढों में गिरते हुए देखा है। यूं तो राजनीति को इन गड्ढों में गिराने में कमोबेश सभी राजनीतिक दल शामिल रहे हैं लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी।शिव सेना ने कम सीट जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी विचारधारा वाली भाजपा को छोडक़र कांग्रेस और एन सी पी के साथ सरकार बनाई थी। लगता है इस चुनाव में तमाम भविष्यवाणियों को धता बताते हुए महाराष्ट्र के मतदाता ने इन तीनों दलों का पत्ता साफ कर दिया। राजनीति में चाल चरित्र और चेहरे का अपना पुराना चोगा बदल चुकी मोदी और शाह के नेतृत्व की बी जे पी ने भी शिवसेना की प्रतिक्रियावश न केवल शिवसेना के दो टुकड़े कर दिए साथ ही उसका साथ देने वाले शरद पवार की एन सी पी को भी दो फाड़ कर दिया। उम्मीद तो यह की जा रही थी कि शिव सैनिक और पवार समर्थक बी जे पी से इसका बदला लेंगे। लेकिन मतदाताओं ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार की शिवसेना और एन सी पी को अवसरवादी गठबंधन करने की सजा दी है।
उद्धव ठाकरे परिवार और शरद पवार परिवार के लिए यहां से वापसी करना वैसा ही मुश्किल होगा जैसा पंजाब में अकाली दल के लिए साबित हो रहा है।भारतीय जनता पार्टी अब महाराष्ट्र में दबंगई के साथ बड़े भाई जैसा व्यवहार कर सकेगी। केंद्र सरकार की छत्रछाया में चलने वाले उसके शासन में अजित पवार और एकनाथ शिंदे की बैशाखियां आने वाले समय में ज्यादा अड़चन नहीं डाल सकेंगी। इस चुनाव में जनता ने यह भी जनादेश दिया है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गठबंधन बेमेल है। दोनों दलों की विचारधारा में धरती आसमान का फर्क है शायद इसीलिए इन दोनों पुराने दलों को महाराष्ट्र की जागरूक जनता ने सिरे से नकार दिया।
महाराष्ट्र का महत्व अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। देश की आर्थिक राजधानी होने से इस राज्य में हर राजनीतिक दल सत्ता चाहता है। यही कारण था कि महाराष्ट्र चुनाव में शामिल प्रत्येक प्रमुख दल ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। चुनाव परिणाम भी सभी को चौंकाने वाले हैं। शरद पवार को यह उम्मीद नहीं थी कि अपने अंतिम समय में इतने बुरे दिन देखने को मिलेंगे। साफ जाहिर है कि तमाम एग्जिट पोल के विपरीत महाराष्ट्र की जनता ने शरद पवार से भावनात्मक रिश्ता भी खत्म कर दिया। जिस तरह बालासाहब ठाकरे ने भतीजे राज ठाकरे को दरकिनार कर अपने राजनीतिक रूप से अपरिपक्व बेटे उद्धव ठाकरे को गद्दी सौंपकर अपने दल के पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी वैसा ही शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार को दरकिनार कर बेटी सुप्रिया सुले को कमान सौंपकर एन सी पी का नुकसान किया है। इस चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिव सैनिक विरासत और शरद पवार का चाणक्य का खिताब धूल में मिल गया। इंडिया गठबंधन और विशेष रूप से कांग्रेस इस चुनाव में उसी तरह पस्त हुई है जैसे हरियाणा में हुई थी। लगता है कि कांग्रेस को जनता से ज्यादा विश्वास एग्जिट पोल पर होने लगा है। उसे एंटी इनकंबेंसी फैक्टर को भुनाने की कला अच्छे से सीखने की आवश्यकता है अन्यथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह वह अन्य राज्यों में भी पिछड़ती चली जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस के लिए महाराष्ट्र की जीत बेहद खास है। यहां भाजपा को इतनी सीट राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय होने के बावजूद पहले कभी नहीं मिली थी। भाजपा अकेले बहुमत के आंकड़े से थोड़ा कम तक पहुंच गई इसलिए वह गठबंधन में मुख्यमंत्री पद के लिए सशक्त दावेदार है। पिछली बार भाजपा और देवेंद्र फडणवीस की काफी छीछालेदार हुई थी जब पहले उन्हें अजित पवार ने गच्चा दिया था और बाद में मुख्यमंत्री से उपमुख्यमंत्री बनना पड़ा था। अब भाजपा अच्छे से ड्राइविंग सीट पर काबिज हो गई।
-नितिन श्रीवास्तव
शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के आए नतीजों में ‘महायुति’ गठबंधन ने ज़बर्दस्त जीत हासिल की है, जिसमें सबसे अहम किरदार बीजेपी का रहा।
149 सीटों पर चुनाव लडऩे वाली भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 132 सीटें जीतने में कामयाब हुए, यानि बीजेपी के कऱीब 90 फ़ीसदी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है।
इस जीत के पीछे मौजूदा ‘महायुति’ सरकार की मुख्यमंत्री ‘लाडकी बहिन’ योजना और प्रदेश में किसानों के लिए सब्सिडी के अलावा विकास के कार्यों पर तो विस्तार से बात भी हो रही है और विश्लेषण भी।
लेकिन इस जीत के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को समझने की भी ज़रूरत है।
1. नारों को मतदाताओं तक पहुँचाना
करीब एक महीने पहले महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव प्रचार अपने शबाब पर था।
भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों में से एक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मैदान में उतार रखा था और उन्होंने ‘बंटेंगे तो कटेंगे’ वाला एक विवादित नारा भी दे दिया था।
मुंबई और कुछ दूसरे शहरों में ये नारे वाले पोस्टर रातोंरात लग गए थे और राज्य में कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इसे ‘सांप्रदायिक और भडक़ाऊ’ करार दे दिया था।
नारे पर छिड़े विवाद के महज तीन दिन बाद नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर में इस पर चर्चा चल रही थी। निष्कर्ष साफ था। बीजेपी को किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर नहीं होने देना है।
आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने अगले दिन कहा, ‘कुछ राजनीतिक ताकतें हिंदुओं को जाति और विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगी और हमें न सिर्फ इससे सावधान रहना है बल्कि इसका मुकाबला करना है। किसी भी कीमत पर बंटना नहीं है।’
संदेश शायद बीजेपी तक भी पहुंच चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया नारा दिया, ‘एक हैं तो सेफ़ हैं’। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे योगी आदित्यनाथ के नारे से जोड़ते हुए मगर ज़्यादा ‘असरदार’ बताया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्तर्गत काम करने वाले तमाम संगठनों में से दो ‘लोक जागरण मंच’ और ‘प्रबोधन मंच’ को इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि वे घर-घर जाकर ‘एक हैं तो सेफ़ हैं’ वाले नारे का न सिर्फ मतलब समझाएं बल्कि ‘हिंदुओं को आगाह करें कि अगर वे संगठित नहीं रहे तो उनका अस्तित्व ख़तरे में पड़ सकता है।’
‘बिजऩेस वल्र्ड’ पत्रिका और ‘द हिंदू’ अख़बार के लिए लिखने वाले राजनीतिक विश्लेषक निनाद शेठ का मानना है, ‘एक नारा अगर धार्मिक तजऱ् पर था तो दूसरा अन्य पिछले वर्गों को एकजुट करने की मंशा वाला। नारों के मतलब सभी ने अलग-अलग निकाले लेकिन वो आम वोटर जो टीवी और सोशल मीडिया से दूर हैं उस तक संदेश पहुंच गया, ऐसा लगता है’।
2. कोर टीम
इसी साल लोक सभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली ‘महायुति’ महाराष्ट्र की 48 लोक सभा सीटों में से महज 17 जीत सकी थी।
राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी के मुताबिक, ‘लोक सभा चुनाव में न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि दूसरे बड़े राज्यों में भी आरएसएस काडर कम नजऱ आ रहा था।’
बीजेपी को इसका एहसास बखूबी रहा क्योंकि इस चुनाव में पार्टी ने न सिर्फ आरएसएस पर अपनी निर्भरता की बात दोहराई बल्कि चुनाव से जुड़े शीर्ष नेतृत्व को भी ध्यान से चुना गया।
महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने चुनावों से पहले ही कह दिया था, ‘हमने वोट जिहादियों और अराजकतावादियों से लडऩे के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद ली है।’
देवेंद्र फडणवीस नागपुर के रहने वाले हैं जो आरएसएस का गढ़ है और उनके पिता गंगाधर फडणवीस स्वयंसेवक होने के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी भी थे, जिन्हें बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपना ‘राजनीतिक गुरु’ भी मानते हैं।
बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव में कुछ वैसा ही किया जो उसने हरियाणा में किया था। हरियाणा में चुनाव इंचार्ज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होकर उभरे धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी गई थी।
महाराष्ट्र में कमान भूपेन्द्र यादव और अश्विनी वैष्णव को दी गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने नाम न लिए जाने की शर्त पर बताया, ‘वैष्णव ब्यूरोक्रैट रहे हैं और महाराष्ट्र जैसे धनी और फैले हुए राज्य में कैंपेन को ऑर्गनाइज करना ऐसे लोगों को बखूबी आता है। लेकिन भूपेन्द्र यादव का वहां चुनाव इंचार्ज बनना एक बड़ा फैसला था जिसमें आरएसएस से पक्का बात की गई होगी।’
उन्होंने आगे बताया, ‘पेशे से वकील भूपेन्द्र, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के महासचिव रह चुके हैं जिसे ‘आरएसएस लॉयर्स विंग’ के नाम से जाता है। कम लोगों को पता होगा कि बीजेपी के संगठन में उन्हें पहली बार जगह देने वाले ख़ुद नितिन गडकरी हैं जिन्होंने साल 2010 में अपने अध्यक्ष-पद पर कार्यकाल के दौरान भूपेन्द्र यादव को पहली बार महासचिव बनाया था।’
इसके अलावा आरएसएस ने अपने पश्चिमी प्रांत के प्रमुख रहे अतुल लिमये को बीजेपी नेताओं बीएल संतोष और बीजेपी और आरएसएस के बीच कोऑर्डिनेटर अरुण कुमार के साथ मिलकर काम करने के लिए भी कहा।
नतीजों में जीत हासिल होने के बाद आप में से बहुतों ने देवेंद्र फडणवीस को पार्टी के वरिष्ठ नेता और आरएसएस के सबसे करीब बताए जाने वाले नितिन गडकरी के घर जाकर उन्हें मुबारक़बाद देते हुए भी देखा ही होगा।
लेकिन इस बात पर भी ग़ौर करना ज़रूरी है कि साल 2014, 2019 और 2024 के लोक सभा चुनावों में जहां नितिन गडकरी पर कैंपेन का दायित्व कम दिया गया। वहीं इस बार महाराष्ट्र में उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। प्रचार खत्म होने के आखिरी 20 दिनों में ही उन्होंने 70 से ज़्यादा चुनावी रैलियाँ कीं।
‘द हितवाद’ अख़बार के राजनीतिक संवाददाता विकास वैद्य बताते हैं, ‘ये एक संदेश भी था उस पुराने आरएसएस-बीजेपी वोटर के लिए कि सब साथ आओ, मिलकर दोबारा सरकार बनाओ जिसमें बीजेपी का सबसे अहम रोल रहे।’
3. शहरी मतदाताओं पर फोकस
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दो प्रांत प्रचारकों से बात करने पर एक ‘टीस’ साफ दिखती है।
2024 लोक सभा चुनावों में बीजेपी का ‘अबकी बार 400 पार’ का नारा ‘अपने तमाम मतदाताओं को एक ऐसे कम्फर्ट जोन में ले गया कि वे घरों से वोट करने ही नहीं निकले’।
इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के छोटे-बड़े शहरों में आरएसएस ने अपनी शाखाओं के जरिए पिछले चार महीने से ‘डोर-टू-डोर कैंपेन’ चलाकर लोगों को बीजेपी सरकार के ‘स्थायी विकास’ वाली बात को पहुँचाने में मदद की।
महायुति के गठन में अजित पवार के आने से संघ बहुत खुश नहीं था लेकिन इस चुनाव में आरएसएस के लोग भी इस बात को भूल कर मुद्दों को लोगों तक पहुंचा रहे थे।
पिछले लोक सभा चुनाव में हुए ‘औसत प्रदर्शन’ को इससे जोड़ कर देखने वाले संघ ने इस चुनाव में उसे दूर करने के लिए पार्टी को बधाई देते हुए अपनी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में लिखा है, ‘लाडकी बहन’ योजना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में माओवाद से निपटना और किसानों के हित की बात करना इस बार कारगर साबित हुआ।’
शहरी मतदाताओं और मध्यम वर्गीय वोटरों पर फोकस दोबारा लाने का ही नतीजा था कि इस चुनाव ने साल 1995 के बाद से 66.05 फीसदी यानी सबसे ज़्यादा मतदान दर्ज किया।
‘द इकनॉमिक टाइम्स’ अखबार के लिए बीजेपी और आरएसएस कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार राकेश मोहन चतुर्वेदी के मुताबिक़, ‘अर्बन या शहरी वोटरों पर आरएसएस का फ़ोकस ठीक वैसा ही था जैसा साल 2014 के आम चुनावों में देखने को मिला था।’
‘इस तरह की वन-टू-वन कैंपेन में आपको कभी कोई भी किसी झंडे और बैनर या लाउडस्पीकर के साथ नहीं दिखेगा। बस आपके मोहल्ले या बूथ के आसपास का कोई व्यक्ति आपसे अक्सर मिलेगा और अपनी बात को बहुत आहिस्ता से बता देगा, जैसे रोज़मर्रा की मुलाक़ात होती है, बस।’
उन्होंने आगे बताया, ‘लेकिन खास बात ये होती है कि इस तरह की कैंपेन जाति, धर्म या वर्ग से परे होती है। और जिस तरह बीजेपी ने सीटें जीती हैं वो इस बात को साफ दर्शा रही है।’
4.संघ प्रबंधन का रोल
इस लोक सभा चुनाव में प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन से निराश आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व ने इस बार पहले से ही ‘अपना होमवर्क कर रखा था।’
नागपुर में ‘द हितवाद’ अखबार के राजनीतिक संवाददाता विकास वैद्य के अनुसार, ‘बहुत जमाने बाद मैंने संघ के स्तर पर इस तरह की माइक्रो-प्लानिंग देखी, जिसके तहत प्रदेश के बाहर से करीब 30 हजार लोगों को चुनाव में मदद के लिए अलग-अलग समय पर बुलाया गया।’
दरअसल पिछले लोक सभा चुनाव के औसत प्रदर्शन के बाद आरएसएस ने राज्य के हर जि़ले में एक कमेटी बनाई थी जिसने लोगों से मिलकर ये टोह लिया कि प्रदेश की महायुति सरकार में और क्या बेहतरी की जा सकती है। इस काम के लिए देश के कई राज्यों से संघ में काम करने के लिए लोग बुलाए गए, जिसमें पुरुष और महिलाएँ दोनों शामिल थे।
खास बात ये थी कि इसमें उत्तर में बीजेपी शासित राज्य जैसे; यूपी और मध्य प्रदेश के अलावा गैर बीजेपी-शासित राज्यों के लोगों को भी बुलाया गया जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैस राज्यों से भी आए।
विकास वैद्य के मुताबिक, ‘इन लोगों ने छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में दौरे किए और मतदाताओं को बताया कि दूसरे राज्यों में जहां कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी की भी सरकार है, वे कैसे अपने चुनावी वादों को भूल जाते हैं, जबकि बीजेपी महाराष्ट्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए कटिबद्ध है और इसका उदाहरण है 'लाडकी बहन योजना' से आने वाले पैसा।’
नागपुर में वरिष्ठ पत्रकार भाग्यश्री राउत के अनुसार, ‘प्रचार के इस प्रोग्राम के तहत वोटरों को तीन श्रेणी में बांटा गया- कैटेगरी ‘ए’ में पारंपरिक बीजेपी वोटरों को रखा गया, मगर कैटेगरी ‘बी’ और ‘सी’ में निशाना उन वोटरों को बनाया गया जो बीजेपी के पक्के वोटर नहीं रहे थे।’
उन्होंने आगे बताया, ‘धीमे स्वर में ही सही लेकिन प्रचार ऐसे मुद्दों पर हुआ कि आखिर ‘देश के लिए राम मंदिर किसने बनवाया या बाबा साहेब आंबेडकर को भारत रत्न किस सरकार ने दिया था।’ (bbc.com/hindi)
-प्रियंका जगताप
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले ‘महायुति’ गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है।
राज्य की 230 विधानसभा सीटें जीतते हुए ‘महायुति’ ने कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार गुट) और शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गुट के महाविकास अघाड़ी गठबंधन को महज 50 सीटों पर रोक दिया है।
कुल 288 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 132, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 और अजीत पवार की एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं।
विश्लेषकों का मानना है कि इस ‘अप्रत्याशित जीत’ के पीछे सबसे बड़ी वजह महाराष्ट्र में ‘मुख्यमंत्री- मेरी लाडली बहन’ योजना रही है।
महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने इस साल जून महीने में यह योजना शुरू की थी।
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं।
राज्य में करीब दो करोड़ लाभार्थी महिलाएं हैं। विश्लेषकों के मुताबिक इस वर्ग ने ‘महायुति’ सरकार को सत्ता में लाने का काम किया है।
मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में प्रयोग
महायुति सरकार ने अपने बजट में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की घोषणा की थी।
योजना की घोषणा के बाद महायुति सरकार की तरफ से बार-बार कहा गया कि यह विधानसभा चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी।
क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने साल 2023 में मध्य प्रदेश में ‘लाडली बहन योजना’ की शुरुआत की थी।
तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तब महिला वोटरों को गोलबंद करने के लिए एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते खोले थे।
मध्य प्रदेश सरकार ने 23 से लेकर 60 साल तक की उम्र वाली महिलाओं के खाते में प्रति माह 1000 रुपये की रकम ट्रांसफर करना शुरू किया था। हालांकि अब ये राशि राज्य सरकार ने बढ़ा दी है।
मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने इसे महाराष्ट्र में भी लागू किया।
क्या कहते हैं विश्लेषक
वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी का मानना है कि 'मुख्यमंत्री- मेरी लाडली बहन' योजना ने आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ गुस्से को कम करने का काम किया है।
वे कहते हैं, ‘लोकसभा चुनाव के बाद महंगाई को लेकर किसानों के साथ-साथ आम लोगों में बहुत गुस्सा था, लेकिन जब मां या बहन के खाते में पैसा आता है, तो वह सीधा घर में दिखाई देता है। ऐसे में गुस्सा अपने आप कम हो जाता है।’
सुधीर कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद एनसीपी के अजित पवार भी लाडली बहन योजना को गेम चेंजर बता चुके हैं।
इस योजना के असर पर बात करते हुए वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता प्रतिमा परदेशी कहती हैं कि इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है।
वे कहती हैं, ‘इस चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ा है, इसलिए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसके पीछे लाडली बहन योजना का असर हो सकता है।’
परदेशी कहती हैं, ‘अगर इस योजना की सिर्फ एक किस्त ही मिली होती तो ऐसा नहीं कहा जा सकता था, लेकिन चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में तीन किस्त जमा की गईं, जिसका परिणाम यह हुआ कि मतदान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी।’
वे कहती हैं, ‘ऐसा लगता है कि इस योजना से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं प्रभावित हुई हैं। शहर के मध्यम वर्ग और गरीब तबके की महिलाओं को भी पैसा मिला है, क्योंकि महायुति सरकार ने अब तक इस योजना के लिए कोई खास मानदंड निर्धारित नहीं किए हैं।’
‘इस योजना का असर यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं यह भी भूल गईं कि उन्हें उनकी सोयाबीन की फसल की कीमत नहीं मिली थी।’
महिला वोटरों की संख्या में बढ़ोतरी
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक महाराष्ट्र में पहली बार महिला मतदाता इतनी बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकलीं।
चुनाव प्रचार के दौरान महायुति सरकार की तरफ से बार-बार कहा गया कि अगर वे सत्ता में दोबारा से चुनकर आते हैं तो लाडली बहन योजना की राशि को बढ़ाया जाएगा।
अजित पवार की एनसीपी ने भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर इस योजना का खूब प्रचार किया।
इसका असर यह हुआ है कि कई महिलाओं को पहली बार पैसा मिला और लाखों की संख्या में महिलाओं ने पहली बार बैंक खाते खोले।
प्रतिमा परदेशी कहती हैं कि इस योजना से खासकर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के हाथ में पैसा आया जिससे उनमें सशक्तिकरण की भावना पैदा हुई और मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई।
जानकारों का कहना है कि दिवाली से एक दिन पहले महिलाओं के खाते में पैसा डाला गया जिससे इस योजना का काफी चर्चा हुई। (bbc.com/hindi)
गौतम अदानी पर अमेरिका में लगे आरोपों का असर भारत से लेकर कीनिया तक में स्पष्ट दिखा।
कीनिया ने गुरुवार को अचानक अदानी समूह से नैरोबी एयरपोर्ट के विस्तार और ऊर्जा सेक्टर के कऱार को रद्द करने का फैसला किया।
अदानी समूह के प्रोजेक्ट को लेकर नैरोबी में काफी विवाद था।
अगर कीनिया में अदानी समूह को एयरपोर्ट विस्तार की डील मिल जाती तो उन्हें 30 साल के लिए नैरोबी एयरपोर्ट के संचालन की जि़म्मेदारी मिलती।
नैरोबी एयरपोर्ट के वर्कर अदानी के साथ इस डील का विरोध कर रहे थे। इन्हें डर था कि एयरपोर्ट के संचालन का काम अदानी को मिलेगा तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है।
कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रुटो ने गुरुवार को अदानी से कऱार रद्द करने की घोषणा की तो कई तरह के सवाल उठने लगे।
कीनिया में एयरपोर्ट के वर्कर के साथ वहाँ का विपक्ष भी अदानी से कऱार को लेकर राष्ट्रपति विलियम रुटो को निशाने पर ले रहा था।
कीनिया के एक्टिविस्ट नेता मोरारो केबासो ने इसी साल 31 अगस्त को अपने एक्स अकाउंट पर लिखा था, ‘भ्रष्ट भारतीय आखिरकार यहाँ आ ही गए। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये सब हो रहा है। हमारे राष्ट्रपति जो कीनिया से बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्होंने 30 साल के लिए एयरपोर्ट अदानी को दे दिया है। अदानी सुन लीजिए अगर 2027 में हम राष्ट्रपति चुने गए तो आपको यहाँ से भागना होगा। हम भ्रष्टाचार से नफरत करते हैं, इसलिए आपसे भी नफऱत करते हैं।’
करार रद्द होने के बाद भी सवाल
कीनिया के राष्ट्रपति ने भले अदानी से कऱार रद्द करने की घोषणा की है लेकिन वहाँ के मीडिया में कई और सवाल पूछे जा रहे हैं।
कीनिया के मशहूर अंग्रेज़ी अख़बार नेशन ने लिखा है कि अदानी के साथ कीनिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी 79 करोड़ डॉलर की डील की है लेकिन राष्ट्रपति ने इस पर चुप्पी साध रखी है।
गुरुवार को कीनिया के कुछ नेताओं ने वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ अदानी की डील को लेकर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। कीनिया के सीम से सांसद डॉ जेम्स नैकल जो कि वहाँ की संसद में हेल्थ कमेटी के सदस्य भी हैं, उन्होंने कहा कि सरकार अदानी के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय से हुई डील पर चुप है।
हालांकि कीनिया के मीडिया में अदानी से करार रद्द करने को राष्ट्रपति विलियम रुटो का मजबूरी में लिया गया साहसिक फैसला बताया जा रहा है।
अदानी एनर्जी सॉल्युशन ने अक्तूबर में लगभग 74 करोड़ डॉलर की डील कीनिया इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी से की थी।
इसके तहत अदानी समूह को चार ट्रांसमिशन लाइन और दो सबस्टेशन बनाने थे। इसके एवज में अदानी समूह को 30 साल के संचालन की जिम्मेदारी मिलती।
इसके अलावा अदानी समूह एक और डील फाइनल करने के करीब था। यह डील कीनिया एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ एक अरब 82 करोड़ डॉलर की थी।
इसके तहत अदानी समूह को जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार करना था। कहा जा रहा है कि कीनिया ने भले कऱार रद्द करने की घोषणा की है लेकिन उसे इसकी क़ीमत चुकानी पड़ सकती है क्योंकि यह डील फाइनल थी और इसे तोडऩे का मतलब कानूनी अनुबंधों का पालन नहीं करना होगा।
भारत के लिए झटका
कीनिया के इस फैसले को कई लोग भारत के लिए झटके के रूप में देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि अदानी का विदेशों में पाँव जमाना भारत के वैश्विक उभार से सीधा जुड़ा है।
दक्षिण एशिया में भारत को चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड में भूटान को छोडक़र भारत के सारे पड़ोसी देश शामिल हैं।
अंतरराष्ट्रीय मामलों का जानकार कांति बाजपेयी भी तर्क देते रहे हैं कि चीन का सामना करने के लिए भारत को अदानी जैसे प्राइवेट फर्म की जरूरत है। अदानी के वैश्विक उभार को भारत के वैश्विक आर्थिक प्रभाव से जोड़ा जाता रहा है।
कीनिया के करार रद्द करने पर भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने लिखा है, ''बांग्लादेश की तरह अमेरिका ने कीनिया में भारत के हितों को झटका दिया है। कीनिया ने अदानी से करार रद्द कर चौंकाया है। यह चीन के लिए है।’
कंवल सिब्बल कहना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में भारत की पसंद वाली शेख़ हसीना की सरकार थी और अमेरिका को यह रास नहीं आ रहा था। अमेरिका शेख हसीना को लगातार मानवाधिकार और लोकतंत्र को लेकर घेर रहा था।
अमेरिका पर शक
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद युनूस को बाइडन प्रशासन का पसंदीदा बताया जाता है लेकिन उनके आने से भारत की असहजता बढ़ी है।
सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘अदानी और अन्य पर कथित रिश्वत का मामला भारत में हुआ है लेकिन इन पर आरोप अमेरिका में तय हो रहा है। अमेरिका चाहता है कि वो अपने क़ानून के हिसाब से कार्रवाई करे क्योंकि अदानी ने अमेरिकी निवेशकों से पैसे जुटाए थे। निज्जर और पन्नू केस की तरह मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है।’
कंवल सिब्बल ने पूरे मामले को लेकर लिखा है, ‘अदानी पर आरोप है कि वह कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों की सरकारों वाले राज्यों में रिश्वत के मामले में शामिल थे। रिश्वत का आरोप भारतीयों पर है न कि अमेरिकी नागरिकों पर। कथित भ्रष्टाचार भारत में हुआ है।’
‘किसी भी तरह की जांच भारत में होना चाहिए। जो अमेरिका में प्रभावित हुए हैं, उन्हें भारत की न्यायिक व्यवस्था में आना चाहिए। यह मामला अमेरिका के न्यायिक अधिकार क्षेत्र का नहीं है। जब तक अमेरिका में कोई भारतीय अपराध नहीं करता है, तब तक उसे अमेरिकी न्यायिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अमेरिकी न्यायिक व्यवस्था का बहुत ही राजनीतिकरण हो चुका है।’
अदानी के प्रोजेक्ट को लेकर कीनिया के अलावा श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश में भी विवाद हो चुका है।
जून 2022 में श्रीलंका के सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) के अध्यक्ष ने संसदीय समिति के सामने ये बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश में एक बिजली परियोजना अदानी समूह को दिलवाने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर 'दबाव' बनाया था।
सीईबी चेयरमैन एम.एम.सी फर्डिनांडो ने साल 2022 में 10 जून को सार्वजनिक उद्यमों पर संसद की समिति को बताया था कि मन्नार जि़ले में एक विंड पावर प्लांट का टेंडर भारत के अदानी समूह को दिया गया। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर ये सौदा अदानी समूह को देने के लिए दबाव बनाया गया था।
फर्डिनांडो ने संसदीय समिति को बताया था कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने उन्हें कहा था कि ये टेंडर अदानी समूह को दिया गया है क्योंकि ऐसा करने के लिए भारत सरकार की ओर से दबाव है।
संसदीय समिति के सामने फ़र्डिनांडो ने कहा था, ‘राजपक्षे ने मुझे बताया था कि वो मोदी के दबाव में हैं।’ हालांकि अदानी समूह ने इन आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया था। (bbc.com/hindi)
-ओक्साना तोरोप
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि यूक्रेन में जारी जंग वो ‘एक दिन में’ खत्म कर देंगे।
चूंकि यूक्रेन को एटीएसीएमएस टैक्टिकल मिसाइलों और एंटी-पर्सनल माइन्स के इस्तेमाल की अनुमति मिलने के बाद सीमावर्ती के बिगड़े हालात को और बढ़ा दिया है, तुरंत शांति समझौते के लिए क्या संभावनाएं हैं?
अपने चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं बताया कि वो इस युद्ध को कैसे खत्म करेंगे। कई विश्लेषकों का ये मानना है कि इस संघर्ष को खत्म करने के लिए अभी भी योजना बनाई जा रही है।
कीएव को उम्मीद है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के शुरुआत होते ही यूक्रेन और रूस से समझौते की बात करेंगे।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 'राजनयिक तरीकों से' 2025 में युद्ध खत्म करने का इरादा जताया है।
लेकिन यह वक्त का क्या मतलब है, ऐसी बातचीत से क्या नतीजों की संभावना है और 1,000 किलोमीटर की सीमा रेखा पर क्या हो रहा है, जिससे कोई संभावित समझौते को प्रभावित कर रहा है?
आगे बढ़तीं रूसी सेनाएं
सीमा रेखा के साथ-साथ लड़ाई के मैदान में हालात रूस के पक्ष में झुकती रही है।
रूसी सेनाएँ पूर्वी डोनबास क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, साथ ही उत्तर-पूर्व में खार्किव क्षेत्र के कुप्यंस्क शहर और दक्षिण-पूर्व में एक बड़े क्षेत्रीय केंद्र ज़ापोरिजि़्जय़ा शहर की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
अक्टूबर में रूस ने यूक्रेनी क्षेत्र के अतिरिक्त 500 वर्ग किलोमीटर पर कब्ज़ा कर लिया था, मार्च 2022 के बाद से ये सबसे ज़्यादा बढ़त थी।
राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक़, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यूक्रेनी क्षेत्र का 27 फ़ीसदी हिस्सा अब रूस के कब्ज़े में है। इसमें क्रीमिया और 2014 में कब्जा किए गए देश के पूर्वी का हिस्सा शामिल है।
मॉस्को कथित तौर पर उत्तर कोरिया के सैनिकों को रूस के कुर्स्क क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है।
अगस्त में यूक्रेन ने सीमा पार से अचानक हमला करके इस क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया था और तब से इसको शांति समझौते के लिए अपने पास रखा है।
कई विश्लेषकों और सैन्य प्रतिनिधियों ने बीबीसी से कहा कि क्रेमलिन युद्धविराम वार्ता के लिए समय पर अधिक यूक्रेनी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की जल्दी में है, क्या उन्हें जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के शुरुआत के तुरंत बाद शुरू करना चाहिए ।
वो मानते हैं कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन डोनेट्स्क और लुहान्स्क क्षेत्रों की सीमाओं तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं, या साथ ही ज़ापोरिजि़्जय़ा जैसी और भी क्षेत्रीय राजधानी पर कब्ज़ा करना चाहते हैं।
क्या एटीएसीएमएस और बारूदी
सुरंग हालात को बदल देंगे?
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के यूक्रेन को युद्ध में लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति युद्ध में एक नया मोड़ ला दिया है।
यूक्रेन को एटीएसीएमएस सिस्टम युद्ध के शुरुआत में दिए गए था और उसने इसका इस्तेमाल क्रीमिया और यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों पर हमला करने के लिए कर रहा है।
दोनों ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यूक्रेनी क्षेत्र हैं, जो फि़लहाल रूस के कब्ज़े में है।
इस हफ़्ते के शुरुआत में राष्ट्रपति बाइडेन ने कीव को रूसी सीमाओं के अंदर हमला करने के लिए अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति दी, जिसे मॉस्को ने वृद्धि और ‘आग में तेल फेंकना’ बताया।
विश्लेषकों का मानना है कि एटीएसीएमएस मिसाइल अपने 300 कीमी अधिकतम रेंज के साथ यूक्रेन को राहत देगा लेकिन बड़े पैमाने पर इस स्थिति को यूकेन की ओर नहीं झुका सकता है।
उनके मुताबिक़ यूक्रेन को टेक्टिकल मिसाइल का इस्तेमाल के अनुमति के बाद रूस सभी संभावित स्थिति के लिए तैयारी कर रहा है और ज़्यादा संभावना है कि अपनी कुछ सुविधाओं को सीमा से कहीं दूर फिर से स्थापित करने का समय है।
माना जाता है कि पहली बार यूक्रेन की ओर से एटीएसीएमएस मिसाइल से जब हमला किया गया। तब वो रूस के 100 कीमी अंदर हुआ, जिसमें एक हथियार भंडारण सुविधा को निशाना बनाया गया था।
अमेरिका ने ये भी घोषणा की कि वो यूक्रेन को बारूदी सुरंग की सप्लाई करने का फैसला लिया है। लेकिन साथ ही अमेरिका ने इसके लिए शर्त रखी है कि इसका इस्तेमाल वो यूक्रेनी इलाके में ही करेंगे और नागरिक आबादी वाली जगहों से दूर किया जाएगा।
इस पूरे युद्ध में रूस खुद के बनाए बारूदी सुरंग का इस्तेमाल करते आया है। लेकिन ये यूक्रेन को अमेरिका से मिले माइन्स से अलग है जो सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए कारगार बनाया गया है, जबकि रूसी बारूदी सुरंग में एक खतरा है जब तक की इसको डिफ्यूज ना किया जाए। पिछले ढाई सालों में बारूदी सुरंग दुर्घटनाओं में करीब 300 यूक्रेनी नागरिकों के मारे जाने की खबर है।
रेड क्रॉस सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन बारूदी सुरंग के खिलाफ़ अभियान चलाते आए हैं।
उनका कहना है कि बारूदी सुरंग अपने पीछे ‘मौत, चोट और पीड़ा की एक लंबे समय तक चलने वाली विरासत छोड़ जाते हैं।’
अब तक यूक्रेन को बारूदी सुरंग देने से अमेरिका झिझकते आया था, लेकिन टैंकों को ध्वस्त करने वाले बारूदी सुरंगों की आपूर्ति करते आया है।
एटीएसीएमएस की तरह, इन हथियारों से यूक्रेनी सैनिकों को आक्रामक होने के बजाय अपनी रक्षा बनाए रखने में मदद मिलने की संभावना है।
लोगों की बदली राय
जबकि सीमा पर युक्रेन के लिए अभी भी चुनौतीपूर्ण जैसे ही हालात हैं, इससे समाज में भी बदलाव आया है। करीब तीन सालों तक उन्हें रोज बम विस्फोट, बिजली कटौती और रातों की नींद हराम होने के कारण यूक्रेन के लोग इस युद्ध से पूरी तरह थक गए हैं और अब उन्हें सर्दियों की चिंता है।
कई सर्वे दिखाते हैं कि रूस से शांति समझौते का विचार लोगों में हावी होने लगा है, चाहे उनको लंबे समय तक अपनी जमीन खोनी पड़े और अनिश्चितता का सामना करना पड़े।
अक्टूबर में थिंक टैंक राजुमकोभ सेंटर ने एक ओपिनियन पोल जारी किया, जो दिखाता है कि तीन में से एक यूक्रेनी बातचीत के पक्ष में है, जो पिछले एक साल पहले पांच में से एक थे।
अक्टूबर में एक और सर्वे के मुताबिक यूक्रेनियों को पक्का विश्वास नहीं है कि उनका देश इस युद्ध के अंत में जीत जाएगा जो हमेशा वो हुआ करते थे, हालांकि अधिकांश लोगों का अभी भी मानना है कि यूक्रेन रूस को इस युद्ध में हरा देगा।
‘ट्रंप प्लान’ का इंतजार
अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद कई पर्यवेक्षक उनके शांति योजना का विवरण सुनने का इंतजार कर रहे हैं।
चुनाव में जीत के बाद दिए गए उनके पहले बयानों से कुछ भी साफ़ नहीं था, जैसे- ‘हम रूस और यूक्रेन के साथ बहुत कड़ी मेहनत करेंगे। इसे रोकना होगा। रूस और यूक्रेन को रुकना होगा।’
अमेरिकी मीडिया ने मुताबिक़ डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बात चीत की, रूसी राष्ट्रपति को चेतावनी दी कि वह युद्ध को नहीं बढ़ाए, लेकिन क्रेमलिन ने इस बात का खंडन किया।
यूक्रेनी विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की योजनी अभी तक पूरी तरह से नहीं तैयार हुई है लेकिन उनकी टीम इसके लिए पहले से ही योजना लेकर आई होगी।
यूक्रेनी विदेश नीति थिंक टैंक ‘न्यू यूरोप’ की निदेशक एलोना हेतमानचुक का मानना है कि इनमें से कई मौजूदा विचार, किसी न किसी तरह से, संघर्ष को ठंडा करने की संभावना है।
हेतमानचुक बताते हैं, ‘युद्ध में सीमा रेखा को स्थिर करना। नाटो में सदस्यता के प्रश्न को रोकना। वित्तीय सहायता को रोकना, कम से कम। बस सब कुछ रोक देना।’
वह इस दृष्टिकोण को बिडेन प्रशासन से बहुत अलग नहीं मानती हैं। अंतर यह है कि डेमोक्रेट्स ने सोचा कि वार्ता की शुरुआत अमेरिका को नहीं बल्कि यूक्रेन को करनी चाहिए, हालांकि उन्होंने यूक्रेन को लंबे समय तक वित्तीय सहायता का भी वादा किया।
लेकिन डेमोक्रेट के विपरीत, ट्रंप ने वार्ता का नेतृत्व करने के लिए एक विशेष यूक्रेन दूत नियुक्त करने का इरादा जाहिर किया है, जिसे कीव एक आशाजनक सकारात्मक के रूप में देखता है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप के पास अमेरिका के दिग्गज राजनयिक कर्ट वोल्कर जैसे प्रतिनिधि थे।
एलोना हेटमनचुक कहती हैं, ‘हमें एक प्रभावशाली ‘मिस्टर यूक्रेन’ की ज़रूरत है जिसकी ट्रंप के कानों तक लगातार पहुंच हो।’
चूंकि यूक्रेन और रूस चल रहे युद्ध के संबंध में नए अमेरिकी प्रशासन के पहले कदम का इंतजार कर रहे हैं, एक बात निश्चित है कि कोई भी संभावित शांति वार्ता जटिल और लंबी होने की संभावना है।
इस संघर्ष के समाधान में दोनों देशों और उनके नेताओं, राष्ट्रपति जेलेंस्की और पुतिन का बहुत बड़ा हित है और उनका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वे किसी भी वार्ता से कितनी अच्छी तरह बाहर निकलते हैं। (bbc.com/hindi)
बाइडेन के यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत देने के बाद रूस ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की अपनी सीमा बदल दी है.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को अपनी परमाणु नीति में बड़ा बदलाव किया. अब रूस कम खतरों पर भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है. यह फैसला तब आया जब अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमला करने की अनुमति दी.
नई नीति के अनुसार अगर रूस पर किसी भी तरह का पारंपरिक हमला होता है और कोई परमाणु शक्ति संपन्न देश उससे जुड़ा हो तो रूस उसका जवाब परमाणु हथियारों से दे सकता है.
ब्रियांस्क पर हमला और बढ़ते खतरे
रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन ने मंगलवार को अमेरिका में बनी एटीएसीएमएस मिसाइलों से रूस के ब्रियांस्क इलाके में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया. इसमें छह मिसाइलें दागी गईं. रूस ने पांच मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन एक मिसाइल जमीन पर पहुंचने में कामयाब रही और उससे नुकसान हुआ. यूक्रेन का कहना है कि उसने रूसी गोला-बारूद के भंडार पर हमला किया.
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस हमले को बड़ा कदम बताया. ब्राजील में जी20 बैठक के दौरान उन्होंने कहा, "अगर यूक्रेन से लंबी दूरी की मिसाइलें रूस पर दागी जाती हैं, तो इसका मतलब होगा कि उन्हें अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों का समर्थन है. हम इसे पश्चिम द्वारा युद्ध का नया चरण मानेंगे और उसका जवाब देंगे.”
परमाणु हथियारों के उपयोग की नई शर्तें
रूस की नई नीति में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए शर्तें बढ़ाई गई हैं. इसमें कहा गया है कि अगर कोई साधारण हमला भी किसी परमाणु देश के समर्थन से होता है, तो इसे रूस पर "साझा हमला" माना जाएगा.
नीति में यह भी कहा गया है कि अगर रूस पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला होता है, तो वह परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है. इसमें बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन जैसे हथियार शामिल हैं.
क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यह बदलाव मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर किए गए हैं. उन्होंने कहा, "पुतिन ने इस साल की शुरुआत में नीति को मौजूदा स्थिति के मुताबिक बदलने का आदेश दिया था.”
पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया
अमेरिका ने रूस की नई नीति की आलोचना की है. अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि रूस परमाणु हथियारों की धमकी देकर यूक्रेन और दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने भी रूस की आलोचना की. उन्होंने कहा, "यह युद्ध का 1,000वां दिन है. 1,000 दिन से रूस की आक्रामकता जारी है. यूक्रेन के साथ हमारा समर्थन हमेशा रहेगा.”
जर्मनी की विदेश मंत्री अनालेना बेयरबॉक ने भी कहा कि उनका देश रूस से डरने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि यह बदलाव दिखाता है कि रूस के पारंपरिक सैन्य बल नाटो के मुकाबले कमजोर हैं.
चीन से मदद की अपील
जी20 बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से रूस पर दबाव बनाने की अपील की. माक्रों ने कहा कि उत्तर कोरिया के सैनिकों का रूस में जाना स्थिति को और खतरनाक बना रहा है. उन्होंने कहा, "परमाणु संकट रोकने में चीन की बड़ी भूमिका हो सकती है. मैंने शी जिनपिंग से कहा कि वह पुतिन से युद्ध रोकने की अपील करें.”
रूस की नई नीति से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है. नई नीति में यह स्पष्ट नहीं है कि रूस कब और कैसे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा. लेकिन यह पश्चिमी देशों को डराने और यूक्रेन को मिलने वाली मदद रोकने की कोशिश है.
फरवरी 2022 से जारी रूस-युक्रेन युद्ध को अब 1,000 दिन से ज्यादा हो गए है. नाटो देश सीधे युद्ध में नहीं उतर रहे, लेकिन वे यूक्रेन को हथियार और समर्थन दे रहे हैं. नई नीति ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है कि अगर कोई गलत कदम उठा लिया गया, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं.
वीके/एए (एपी, रॉयटर्स)
भारत ने जेलों की भीड़ कम करने के लिए एक बड़े कदम का एलान किया है. सरकार ने ऐसे कैदियों को रिहा करने की घोषणा की है, जो अपनी संभावित सजा का एक तिहाई हिस्सा काट चुके हैं.
 डॉयचे वैले पर विवेक कुमार का लिखा-
डॉयचे वैले पर विवेक कुमार का लिखा-
गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की धीमी न्याय प्रक्रिया से निपटने के लिए नई पहल की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि छोटे अपराधों के आरोप में जेल में बंद ऐसे कैदियों को जमानत दी जाएगी, जिन्होंने अपनी संभावित सजा का एक-तिहाई हिस्सा काट लिया है।
भारत की अदालतों में लाखों मामले लंबित हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2024 की शुरुआत तक 1,34,799 लोग सुनवाई के इंतजार में जेल में बंद थे, जिनमें से 11,448 पांच साल से अधिक समय से बिना सजा के जेल में हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उनका लक्ष्य एक ‘वैज्ञानिक और तेज’ आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करना है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में कहा, ‘हमारी कोशिश है कि संविधान दिवस (26 नवंबर) से पहले देश की जेलों में ऐसा कोई कैदी न रहे, जिसने अपनी सजा का एक-तिहाई हिस्सा काट लिया हो और उसे अभी तक न्याय न मिला हो।’
हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना केवल गैर-गंभीर अपराधों के लिए होगी। गंभीर अपराधों या कठोर कानून, जैसे ‘अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
संविधान दिवस और न्याय का मुद्दा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले वर्ष संविधान दिवस पर अपने भाषण में जेलों में बढ़ती भीड़ की ओर ध्यान दिलाया था। उन्होंने कहा था, ‘जेलों में बंद ये लोग कौन हैं? ये वे लोग हैं, जो मौलिक अधिकारों, संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों के बारे में कुछ नहीं जानते।’ उन्होंने न्याय की ऊंची लागत को समस्या बताया और तीनों शाखाओं – कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका – से सुलझा हुआ समाधान खोजने की अपील की थी।
विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस और जेल सुधारों के बिना यह समस्या हल नहीं हो सकती। न्यायपालिका में जजों की भारी कमी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मजबूत करने और जमानत के मौजूदा धन-आधारित मॉडल का विकल्प लाने की सख्त जरूरत है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में जेलों में भीड़ पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक थी। 2021 की जेल सांख्यिकी रिपोर्ट बताती है कि 2016 से 2021 के बीच कैदियों की संख्या 9।5 फीसदी घटी, लेकिन विचाराधीन कैदियों की संख्या 45।8 प्रतिशत बढ़ गई।
टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर विजय राघवन ने हाल ही में फ्रंटलाइन पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि आंकड़े साबित करते हैं कि हर कैदी को जेल में रखने की जरूरत नहीं होती और अगर प्रभावी कानूनी मदद और जमानत की पहुंच हो, तो जेलों में भीड़ घट सकती है। उन्होंने बताया कि 85-90 फीसदी कैदी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय से हैं। इनमें से अधिकांश की पारिवारिक आय 10,000 रुपये प्रति माह से कम है।
आदिवासी और अन्य कमजोर वर्ग
आदिवासी प्रथाओं को अक्सर बिना समझे अपराध घोषित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में आदिवासी युवकों को अक्सर पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है, जबकि वे अपनी परंपराओं के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ सहमति से रहते हैं। इसी तरह, पारधी जैसे विमुक्त जनजातियों के लोगों को छोटे अपराधों के लिए हमेशा संदेह की नजर से देखा जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने 1,382 जेलों की अमानवीय स्थिति पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी) की धारा 436 और 436ए का प्रभावी उपयोग शामिल है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने यूटीआरसी (अंडरट्रायल रिव्यू कमेटी) की तिमाही बैठकें आयोजित करने के लिए ढांचा बनाया है। इसके तहत 2023 में 48 फीसदी विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया, जबकि 16 फीसदी दोषियों को रिहाई मिली।
आगे की राह
हालांकि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने यूटीआरसी की सिफारिशों के बावजूद रिहाई की दर में कमी पर चिंता जताई। इसी महीने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि कई बार एक से अधिक एफआईआर, गंभीर अपराध, या विदेशी नागरिकता जैसे कारणों से कैदियों को रिहाई नहीं मिलती।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डी। वाई। चंद्रचूड़ ने इस रिपोर्ट की भूमिका में कहा था, ‘कैदियों के साथ हमारा व्यवहार हमारे मानवाधिकारों और सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है। सम्मानजनक जेलें सिर्फ आकांक्षा नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व हैं।’ उन्होंने पुनर्वास के लिए बेहतर माहौल बनाने पर जोर दिया।
गृह मंत्री अमित शाह की यह पहल जेलों और अदालतों के बीच की खाई को पाटने का एक कदम है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह न्याय व्यवस्था में स्थायी बदलाव लाने का मौका हो सकता है। (dw.com/hi)
दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में से एक गौतम अदानी के लिए गुरुवार का दिन बहुत भारी रहा।
अमेरिका में उनके खिलाफ रिश्वत और और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। अदानी पर अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगा है।
गुरुवार तडक़े जैसे ही यह ख़बर आई तो दुनिया भर के मीडिया में छा गई। भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तो गौतम अदानी की गिरफ्तारी की मांग की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सांठगांठ का आरोप लगाया। जैसे ही शेयर बाजार खुला अदानी समूह से जुड़ी कंपनियों के शेयर 20 प्रतिशत तक गिर गए।
अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स ब्लूमबर्ग के अनुसार, गौतम अदानी के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी के आरोप तय होने के बाद गुरुवार को उनकी कुल संपत्ति में 15 अरब डॉलर की चपत लग गई।
बाज़ार बंद होने तक उनकी कुल संपत्ति कऱीब 72 अरब डॉलर थी जो साल 2023 के अंत में 84 अरब डॉलर थी। पिछले साल तीन जून तक तो उनकी कुल संपत्ति 122 अरब डॉलर तक पहुँच गई थी।
हालाँकि अदानी समूह ने गुरुवार दोपहर एक बयान जारी कर इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं।
अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए अदानी ग्रुप ने गुरुवार को जारी बयान में कहा, ‘अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट और एक्सचेंज कमीशन द्वारा अदानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और हम उनका खंडन करते हैं।’
आरोप अमेरिका में और असर चौतरफा
अमेरिका में लगे आरोपों का असर शेयर मार्केट में उनकी कंपनियों की बदहाली तक ही सीमित नहीं रहा। गुरुवार शाम में अचानक से कीनिया के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने भारतीय अरबपति गौतम अदानी से एयरपोर्ट के विस्तार और ऊर्जा डील को लेकर जो अरबों डॉलर का करार किया था, उसे रद्द करने का फैसला किया है।
कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रुटो ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह फैसला उन्होंने अपनी जांच एजेंसियों और साझेदार देशों की जाँच के बाद मिली सूचना के आधार पर लिया है।
उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। अदानी ग्रुप कीनिया के साथ कऱार पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में था। इसके तहत कीनिया की राजधानी नैरोबी के मुख्य एयरपोर्ट का विस्तार करना था, जिसमें नए रनवे और टर्मिनल बनाने थे। अदानी को इसके बदले में 30 साल के लिए नैरोबी एयरपोर्ट के संचालन की जि़म्मेदारी मिलती।
कीनिया में अदानी से होने वाली इस डील की भी बहुत आलोचना हो रही थी और एयरपोर्ट वर्कर आंदोलन कर रहे थे। एयरपोर्ट वर्करों का कहना था कि अदानी को एयरपोर्ट के संचालन की जि़म्मेदारी मिलने से नौकरी की शर्तें बदल जाएंगी और उनकी नौकरी भी जा सकती है।
ब्लूमबर्ग से अदानी के एक कऱीबी सहयोगी ने बताया, ‘बुधवार शाम तक सब कुछ अच्छा था। अदानी के ग्रीन एनर्जी बिजऩेस ने बॉन्ड सेल के जरिए 60 करोड़ डॉलर जुटाए थे।अहमदाबाद में बिस्तर पर जाने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कार्ड गेम खेला था। गुरुवार तडक़े तीन बजे एक सहकर्मी ने उन तक परेशान करने वाली ख़बर पहुँचाई। उस सहकर्मी ने बताया कि अमेरिका में उनके और कुछ सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप तय हुआ है।’
15 अरब डॉलर की चपत
ब्लूमबर्ग के मुताबिक, ‘चंद मिनटों में अदानी ग्रुप के सीनियर एग्जेक्युटिव्स कॉन्फ्रेंस कॉल पर आए। न्यूयॉर्क में फेडरल प्रॉसिक्युटर्स ने आरोप लगाया है कि अदानी और उनके सहकर्मियों ने अमेरिकी निवेशकों से रिश्वत विरोधी नियमों को लेकर झूठ बोला क्योंकि उन्होंने भारतीय अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर से अधिक की रक़म की रिश्वत देने का वादा किया था।’
‘जब बाकी का भारत सुबह जगा तब तक अदानी पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देने को लेकर ऊहापोह में थे। जब मुंबई में शेयर बाजार खुला तो अदानी समूह की कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिरने लगे। दोपहर होते-होते अदानी समूह ने एक बयान जारी किया और सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अदानी समूह ने पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी।’
ब्लूमबर्ग ने लिखा है, ‘अदानी को लेकर आने वाले महीनों में राजनीतिक विवाद और बढ़ सकता है। प्रत्यर्पण को लेकर तनातनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में जल्द ही अमेरिका की कमान आने वाली है और अगर वह चाहेंगे तो भारत के साथ डील कर सकते हैं।’
‘ट्रंप की नजऱ में भारत और अदानी चीन के एकाधिकार के खिलाफ अहम साझेदार हैं। अदानी से जुड़े मामलों की जानकारी रखने वालों ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया है कि ट्रंप के परिवार के सदस्य अदानी के अहमदाबाद स्थित आवास पर भी गए हैं। ऐसे मामले में अभियोजन में वर्षों तो नहीं लेकिन महीनों लगेंगे और यह ट्रंप के जस्टिस डिपार्टमेंट पर निर्भर करेगा कि उसका रुख क्या होता है।’
ब्लूमबर्ग ने लिखा है, ‘अदानी को लेकर अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है, उसका असर इस ग्रुप तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसका असर वैश्विक बैंकों पर भी पड़ेगा, जो कर्ज मुहैया कराते हैं। इसके अलावा भारत से जुड़ी जो कंपनियां विदेशों में पाँव जमाना चाहती हैं, उनकी साख पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा।’
ब्लूमबर्ग से थिंक टैंक सेंटर फोर स्ट्रैटिजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में इंडिया एंड इमर्जिंग एशिया इकनॉमिक्स के प्रमुख रिक रोसोव ने कहा, ‘मुझे डर है कि इसका असर अदानी के वैश्विक विस्तार पर पड़ेगा। यह मामला भारत में यह चिंता बढ़ा सकता है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश उभरते भारत की गति धीमी करना चाहते हैं।’
भारत पर क्या पड़ेगा असर?
ब्लूमबर्ग ने लिखा है, ‘पिछले कई सालों में वैश्विक निवेशकों और बैंकों ने अदानी समूह में अरबों डॉलर लगाए हैं। आज की तारीख़ में अदानी का कारोबार पोट्स, पावर, रोड से लेकर एयरपोर्ट तक फैला है। अदानी के प्रोजेक्ट वियतनाम से लेकर इसराइल तक में फैले हैं। अदानी ग्रुप की वैश्विक महत्वाकांक्षा को चीन के बेल्ट एंड रोड के समानांतर भारत की प्रॉक्सी के रूप में देखा जाता है।’
वहीं मशहूर अमेरिकी न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, ‘अदानी कोई सामान्य भारतीय अरबपति नहीं हैं। अदानी को भारत की सरकार के विस्तार के रूप में देखा जाता है। अदानी समूह पोर्ट बनाता है और खऱीदता भी है। ऐसा अक्सर भारत सरकार के अनुबंधों या लाइसेंस के जरिए होता है।’
‘अदानी के पावर प्लांट्स हैं और एयरपोर्ट के संचालन की जि़म्मेदारी भी है। अब तो अदानी के पास टीवी न्यूज़ चैनल का भी स्वामित्व है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अदानी का कारोबार भारत के केंद्र में आ गया। जिस तरह से पीएम मोदी ने भारत को विश्व मंच पर केंद्र में लाया उसी तरह अदानी भी केंद्र में आए।’
न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, ‘भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी इसी गर्मी में अदानी के सोलर ऊर्जा प्रोजेक्ट देखने गए थे। गार्सेटी ने देखने के बाद अदानी को प्रेरक व्यक्ति बताया था।
अमेरिकी अख़बार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेशी दौरे में गौतम अदानी भी जाते रहे हैं। दोनों के दौरों में अदानी ग्रुप के कारोबारी समझौते भी हुए हैं। ये समझौते श्रीलंका से लेकर इसराइल तक में हुए हैं। अदानी भारत में पीएम मोदी की ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग नीतियों का पालन करते हैं और इससे उन्हें राजनीति से डील करने में मदद मिलती है। अदानी की कारोबारी कामयाबी को भारत के उभार के रूप में देखा जाता है।’
वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, ‘अदानी पर अमेरिका में लगे आरोपों से भारत और अमेरिका के संबंध जटिल हो सकते हैं। हाल के वर्षों में अदानी को भारत के भीतर काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। ख़ास करके पीएम मोदी से संबंधों को लेकर। जब भी अदानी मुश्किल में घिरते हैं तो बीजेपी उनके साथ हो जाती है और अदानी की आलोचना करने वालों को भारत का दुश्मन बताती है।’
वॉशिंगटन पोस्ट से ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन में साउथ एशिया प्रोग्राम के डायरेक्टर मिलन वैष्णव ने कहा, ‘बाइडन प्रशासन उम्मीद कर रहा था कि वह भारत के साथ संबंधों को ऊंचाई पर ले जाकर छोड़े। जाहिर है कि इस वाकये से मोदी का मूड खराब हुआ होगा।’ (bbc.com/hindi)
-डॉ. आर.के. पालीवाल
दिल्ली की मुख्यमंत्री के बयान से पराली जलाने पर भी ओछी राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली निवासी पहले दिल्ली के प्रदूषण को पंजाब की पराली के मत्थे मढ़ा करते थे। अब पंजाब में आप सरकार बनने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के किसानों को पराली जलाने का दोषी ठहराया है।पंजाब और हरियाणा सिंचाई की अच्छी व्यवस्था और ठीक-ठाक बारिश की बदौलत खरीफ सीजऩ में खूब धान उगाते हैं और धान की पराली ठिकाने लगाने के लिए उसे जलाना सबसे आसान मानते हैं। पशुपालन कम होने और मजदूरों के अभाव में पराली जलाना ही उन्हें सबसे उचित समाधान नजऱ आता है।
हमारी सरकारों को समस्याओं के सही और सकारात्मक समाधानों के लिए न समय है और न इस मामले में वे अनुभवी विशेषज्ञों से कोई समाधान मांगते हैं। उन्हें कानून बनाकर और कड़ी पेनल्टी लगाकर इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देने और दूसरे दलों को दोषी बताने के विकल्प सबसे आसान और उत्तम लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कई बार आदेश दिए हैं लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए सरकारों के अपने एजेंडे हैं। वे हर मुद्दे को वोट बैंक की दृष्टि से देखते हैं और समस्या को जड़ से खत्म करने के बजाय बचकाने आरोप प्रत्यारोप लगाकर विपक्षी दलों की सरकारों को समस्या की जड़ बता जनता को भटकाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री का बयान इसी की एक कड़ी है।
दिल्ली में केंद्र सरकार का मुख्यालय है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली की आप सरकार के साथ आए रोज सींग लड़ाते रहते हैं। दिल्ली के बड़े अधिकारियों पर भी केंद्र सरकार का ही शिकंजा है जिसके लिए केंद्र सरकार कभी अध्यादेश जारी करती है और कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ती है लेकिन दिल्ली के प्रदूषण से निबटने के लिए उसने भी कोई ऐसी पहल नहीं की जिससे अन्य महानगरों के लिए कोई आदर्श स्थापित हो सके। दिल्ली के प्रदूषण पर सरकारी विफलता का दाग केंद्र और राज्य सरकार पर संयुक्त रूप से लगा है। जब तक दोनों सरकार कंधे से कंधा मिलाकर इस राक्षसी समस्या का समुचित समाधान नहीं खोजेंगी दिल्ली वासी प्रदूषण से हलाकान होते रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की अपनी सीमाएं हैं। वह सरकारों को निर्देश जारी कर सकता है, डांट फटकार सकता है लेकिन सडक़ पर उतरकर समस्या का समाधान नहीं कर सकता।
दिल्ली के निवासियों को भी अपनी जीवनशैली बदलने की जरूरत है। लोकतंत्र और सभ्य एवं सजग समाज में जनता ही सर्वोपरि है। दिल्लीवासियों को अपने अपने स्तर पर कुछ सकारात्मक प्रयास करने चाहिए। दिल्ली की कालोनियों, बंगलों और सडक़ों पर इतनी कारें रेंगती और पार्क होती हैं कि निकलने की जगह नहीं बचती। इन कारों और स्कूटरों के धुएँ से भी अच्छा खासा प्रदूषण होता है। कंक्रीट की ऊंची ऊंची इमारतें बड़े बड़े पेड़ काटने के बाद खड़ी हुई हैं जो छोटे मोटे पेड़ों की धूप रोककर प्रदूषण कम करने वाले पौधों की क्षमता कम कर रही हैं। सारा दोष गरीब किसानों की पराली पर मढक़र दिल्ली के नागरिक और नेता अपने गुनाहों और अकर्मण्यता पर पर्दा नहीं डाल सकते। प्रकृति को नष्ट भ्रष्ट करने में कमोबेश हम सब नागरिकों का हाथ है। चंद पर्यावरणविद लेख लिखकर, भाषण, सेमिनार कर कुंभकर्णी नींद से सोए लोगों को जगाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन सुविधा भोगी स्वार्थी समाज चेतने की कोई कोशिश ही नहीं करता। राजनीतिक दलों में प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हद दर्जे की संवेदनहीनता है। यही कारण है कि किसी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र या चुनावी भाषण में प्रकृति और पर्यावरण का जिक्र नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यदि बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो सकती है, प्राइवेट कंपनियों का काम ऑन लाइन हो सकता है तब सरकारी कामकाज भी ऑन लाइन किया जा सकता है। यहां तक कि न्यायालयों के कार्य भी काफी हद तक ऑन लाइन हो सकते हैं। दिल्ली वाले कुछ दिन कार और स्कूटर की जगह पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करने की ठान लें तो इससे भी प्रदूषण काफी कम हो सकता है।
-शकील अख्तर
भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपने शस्त्रागार में सैन्य ड्रोन का इजाफा कर रहे हैं।
दोनों की ओर से न केवल कई विदेशी ड्रोन खऱीदे गए हैं, बल्कि ख़ुद भी इस टेक्नोलॉजी को तैयार किया गया है जो बिना पायलट के दुश्मन पर निगरानी रखने, जासूसी करने या लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता रखती है।
एशिया की तीन पड़ोसी परमाणु शक्तियों भारत, पाकिस्तान और चीन की ओर से अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए बिना पायलट उड़ान भरने वाले ड्रोन के इस्तेमाल में तेज़ी देखी गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सेना में व्यापक पैमाने पर ड्रोन के शामिल होने से युद्ध का तरीका बदल गया है और किसी भी विवाद या झड़प की स्थिति में ड्रोन का इस्तेमाल बहुत अधिक होगा।
विशेषज्ञों के अनुसार इन तीनों देशों में बड़े पैमाने पर ड्रोन की मौजूदगी और एक दूसरे के खि़लाफ़ जासूसी और निगरानी में उनका बढ़ता हुआ इस्तेमाल निकट भविष्य में टकराव और तनाव का कारण बन सकता है।
इस रिपोर्ट में हमने यह जानने की कोशिश की है कि परंपरागत प्रतिद्वंद्वी समझे जाने वाले पड़ोसी देश भारत और पाकिस्तान के पास ड्रोन क्षमता कैसी है और हाल के समय में दोनों ने किस तरह की अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स (यूएवी) में इज़ाफ़ा किया है।
भारत के पास पाकिस्तान से अधिक ड्रोन
सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स काफ़ी ऊंचाई पर देर तक उड़ान भरने और रडार में आए बिना ज़मीन पर सेना की गतिविधियों, उनकी तैनातियों, महत्वपूर्ण संयंत्रों, नए निर्माण और सैनिक ठिकानों आदि की प्रभावी निगरानी और विशेष लक्ष्य को भेदने में ज़बर्दस्त महारत रखते हैं।
रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार एक सैन्य ड्रोन तीन बुनियादी काम कर सकता है:
निगरानी करना और प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियों पर नजऱ रखना
जासूसी करना यानी यह देखना कि दूसरी तरफ़ हथियार या सेना कहां तैनात हैं
लक्ष्य को निशाना बनाना और उसे तबाह करना
कई ड्रोन्स यह तीनों काम करते हैं लेकिन कुछ की क्षमता सीमित होती है।
अगर हम ड्रोन्स के लिहाज़ से भारत और पाकिस्तान की सैन्य क्षमता की तुलना करें तो यह पता चलता है कि दोनों प्रतिद्वंद्वी देशों ने हाल के दौरान इसमें वृद्धि की है।
रक्षा मामलों के विश्लेषक राहुल बेदी ने बीबीसी को बताया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही ड्रोन्स की संख्या बढ़ा रहे हैं।
उनका अंदाज़ा है कि भारत के पास अगले दो-चार सालों में लगभग पांच हजार ड्रोन्स होंगे।
उनके अनुसार वैसे तो पाकिस्तान के पास ‘भारत से कम ड्रोन्स’ हैं लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के पास मौजूद ड्रोन्स में विभिन्न क्षमताएं हैं और यह 10 से 11 अलग-अलग बनावट के हैं।
भारत के ड्रोन्स
अगर हम भारत की मिसाल लें तो उसने इस साल अक्टूबर के दौरान अमेरिका से साढ़े तीन अरब डॉलर मूल्य के 31 प्रीडेटर ड्रोन्स खऱीदने का समझौता किया है।
उनके साथ 50 करोड़ डॉलर के उन ड्रोन्स के ज़रिए लक्ष्य को तबाह करने में इस्तेमाल होने वाले बम और लेजऱ गाइडेड मिसाइलें भी खऱीदी जाएंगी।
अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन्स बहुत महंगे हैं। भारतीय मुद्रा में एक ड्रोन की क़ीमत लगभग 950 करोड़ रुपए है।
इन 31 में से 15 ड्रोन्स भारतीय नौसेना में शामिल किए जाएंगे और बाक़ी 16 थल सेना और वायुसेना में बराबर बराबर दिए जाएंगे।
प्रीडेटर ड्रोन्स दुनिया के सबसे कामयाब और ख़तरनाक ड्रोन माने जाते हैं। इनका इस्तेमाल अफग़़ानिस्तान, इराक, सीरिया, सोमालिया और कई दूसरे देशों के ठिकानों और लक्ष्यों को तबाह करने में किया गया था।
भारत इससे पहले इसराइल के ‘हीरोन’ खऱीद चुका है और इसराइल एयरोस्पेस एजेंसी से लाइसेंस के तहत वह अब यह ड्रोन ख़ुद भारत ने बना रहा है।
मई 2020 में लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ सीमा पर तनाव के बाद ड्रोन और ‘यूएवी’ का महत्व भारत में बहुत बढ़ गया है।
इस समय भारत में नौसेना पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि हिंद महासागर में चीनी नौसेना और भारतीय नौसेना के जहाज़ सक्रिय हैं और भारत का ध्यान इस क्षेत्र पर बहुत अधिक है।
टीकाकारों की राय में अमेरिका भी भारत से यही चाहता है कि वह इस क्षेत्र में चीनी नौसेना की गतिविधियों पर नजऱ रखे।
‘साउथ एशियन वॉयसेज़’ नाम की वेबसाइट पर अक्टूबर की शुरुआत में प्रकाशित एक लेख में रक्षा विश्लेषक ज़ोहैब अल्ताफ़ और निमरा जावेद ने भारत और पाकिस्तान की सेना में ड्रोन को शामिल करने और उसके प्रभाव का विश्लेषण किया है।
उस लेख के मुताबिक, ‘भारत के ड्रोन प्रोग्राम का एक अहम पहलू ‘स्वार्म ड्रोन्स’ को शामिल करना है। यह अनआर्म्ड एरियल व्हीकल है और यह बड़ी संख्या में इक_े उड़ते हैं।’
‘यह पेचीदा मिशन पर काम करने के लिए बनाए गए हैं। उन्हें भारत की रक्षा रणनीति, विशेष कर पाकिस्तान की ओर से किसी ख़तरे को नाकाम बनाने का अहम हिस्सा माना जाता है।’
रिपोर्ट में लिखा है कि इसे भारत की फ़र्म 'न्यू स्पेस रिसर्च ऐंड टेक्नोलॉजीज़' ने तैयार किया है।
उनका मानना है, ‘यह ड्रोन्स दुश्मन की रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर परमाणु बम लॉन्च करने वाले प्लेटफ़ॉर्मों को तबाह करने समेत बहुत सारे ड्रोन्स से एक साथ हमला करके कई लक्ष्यों को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं।’
पाकिस्तान की ‘ड्रोन पावर’
रक्षा मामलों के विश्लेषक राहुल बेदी ने बीबीसी को बताया कि पाकिस्तान तुर्की और चीन से ड्रोन्स आयात करता है। हालांकि उसने जर्मनी और इटली से भी ड्रोन्स खऱीदे हैं।
पाकिस्तान ने बर्राक़ और शहपर जैसे ड्रोन्स ख़ुद भी बनाए हैं।
पाकिस्तान के पास तुर्की के आधुनिक ‘बैराक्तर’ ड्रोन्स टीबी टू और एकेंजी हैं जबकि उसने चीन से ‘वैंग लोंग टू’ और ‘सीएच 4’ जैसे ड्रोन्स भी हासिल किए हैं।
साल 2022 के दौरान पाकिस्तान ने फ़्लैगशिप ड्रोन ‘शहपर टू’ बनाया। इस ड्रोन के बारे में बताया गया कि यह एक हज़ार किलोमीटर तक उड़ान भरकर लक्ष्य को निशाना बना सकता है।
यह अपने लक्ष्य को लेजऱ बीम से लॉक करके उसे मिसाइल की मदद से तबाह कर सकता है।
पाकिस्तान ऑर्डनेंस फ़ैक्ट्री की ओर से पहले ‘अबाबील’ के नाम से सर्विलेंस ड्रोन्स बनाए गए थे जिन्हें युद्ध के लिए हथियारों से लैस किया गया था।
ज़ोहैब और निमरा अपने लेख में विश्लेषण करते हुए लिखते हैं, ‘पाकिस्तान की वायु सेना ड्रोन और परंपरागत साधनों से भारत के एस- 400 और पृथ्वी की आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से टारगेट करके भारत की वायु रक्षा प्रणाली को पंगु कर सकता है।’
इधर राहुल बेदी कहते हैं कि कई रक्षा विश्लेषणों के अनुसार पाकिस्तान दुनिया में चौथा या पांचवा ड्रोन पावर माना जाता है। ‘उनके पास बहुत से आधुनिक प्रकार के ड्रोन्स हैं और उनके ड्रोन वायुसेना, थल सेना और कुछ हद तक नौसेना में भी शामिल किए गए हैं। पाकिस्तान की ड्रोन क्षमता बढ़ रही है और इसका फ़ोकस इस क्षमता में लगातार वृद्धि करने पर है।’
उनका कहना है, ‘इन ड्रोन्स की उड़ान भरने की क्षमता लगभग 50 घंटे तक की है। लड़ाकू विमान उन्हें तबाह नहीं कर सकते क्योंकि यह उनकी उड़ान की ऊंचाई की हद से बहुत ऊपर उड़ते हैं।’
वह कहते हैं कि इन आधुनिक ड्रोन्स के कारण पाकिस्तान को काफ़ी हद तक स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल बढ़त मिलती है।
बालाकोट हमले और अनुच्छेद 370
के हटने से स्थिति कैसे बदली है?
इसी तरह ज़ोहैब और निमरा की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में आधुनिक ड्रोन्स का बड़ी संख्या में शामिल होना, क्षेत्र की सैन्य स्थिरता के लिए ख़तरा पैदा कर रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक, ‘जैसे-जैसे ड्रोन सेना की रणनीति का अहम हिस्सा बनता जा रहा है वैसे-वैसे सैन्य टकराव से बचाने और सैन्य संतुलन की परंपरागत व्यवस्था के बिखरने का ख़तरा बढ़ता जा रहा है।’
‘परमाणु हथियार संपन्न दक्षिण एशिया में परमाणु ठिकानों और संपत्तियों समेत लक्ष्यों पर हमला करने की ड्रोन की प्रभावी क्षमता ने किसी युद्ध की स्थिति में तबाही की आशंकाओं को व्यापक कर दिया है।’
सैन्य मामलों की पत्रिका फ़ोर्स के संपादक प्रवीण साहनी कहते हैं, ‘अभी जो ड्रोन्स है वह या तो ज़मीन से गाइड किए जाते हैं या फिर वह हवा यानी सैटेलाइट से गाइड किए जाते हैं। अगर दुश्मन के पास संचार व्यवस्था को जाम करने की क्षमता हो तो वह ड्रोन्स को निष्प्रभावी कर सकता है।’
वह कहते हैं, ‘यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे भारत ने जब बालाकोट स्ट्राइक की थी तो पाकिस्तान के पास वायु संचार प्रणाली को जाम करने की क्षमता थी। उन्होंने भारतीय पायलट की संचार व्यवस्था को जाम कर दिया था। यही वजह थी कि वह पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की तरफ़ उतरा।’
प्रवीण साहनी का कहना है, ‘चीन मिलिट्री टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है। पाकिस्तान को चीन से ड्रोन बनाने की टेक्नोलॉजी मिल रही है। पाकिस्तान के पास आज बहुत अधिक क्षमता है।’
‘पाकिस्तान की वायुसेना बहुत मज़बूत हो गई है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका चीन की है। चीन 10-15 वर्षों से मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। 5 अगस्त 2019 के बाद चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य साझेदारी बहुत मज़बूत हुई है।’
वह कहते हैं, ‘अब जो वॉरफ़ेयर है उसमें फि़जिक़ल फ़ील्ड में यानी जहां-जहां लड़ाई में इंसान काम करते थे वह अब इंसान से मशीन की तरफ शिफ़्ट हो रही है। फि़जिक़ल का मतलब ज़मीन, समंदर, आसमान, समंदर के नीचे और अंतरिक्ष- इन सब में ड्रोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने जा रहा है।’
‘यह विभिन्न देशों में उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग-अलग चरणों में हो रहा है। अभी ड्रोन पूरी तरह संचार व्यवस्था से कंट्रोल किए जा रहे हैं।’
लेकिन साहनी ये नहीं मानते ड्रोन के लिए कोई रेस लगी हुई है। उनका कहना है, ‘यह वॉरफ़ेयर में होने वाले तकनीकी बदलाव का संकेत है। दुनिया अब ड्रोन वॉरफेयर के चरण में है और ड्रोन वॉरफेयर मौजूदा समय और भविष्य का वॉरफ़ेयर है।’
क्या ड्रोन का बढ़ता इस्तेमाल इन देशों के लिए खतरा है?
यूक्रेन और गजा की जंगों में ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल हुआ है। विश्लेषक अजय शुक्ला ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, ‘ड्रोन्स उन जगहों पर अधिक कारगर साबित होते हैं जहां जिस पक्ष पर हमला हो रहा है उसके पास वायु रक्षा प्रणाली बहुत कमजोर हो।’
‘ड्रोन्स का जो इस्तेमाल आप गजा और कई दूसरी जगहों पर देख रहे हैं। वहां जिन पर हमला हो रहा है उनके पास एयर डिफ़ेंस सिस्टम या आर्म्ड एयर फ़ोर्स जोकि ड्रोन से अधिक क्षमतावान हो, मौजूद नहीं।’
‘लेकिन अगर आप भारत और चीन का उदाहरण लें, तो चीन के शस्त्रागार में मौजूद आधुनिक ड्रोन्स भारत के उन्हीं इलाकों में कारगर साबित होंगे जहां कोई एयर फ़ोर्स या लड़ाकू विमान न हों। बाकी जगहों पर वह कामयाब नहीं होंगे।’
उनका कहना है, ‘पाकिस्तान, चीन या भारत में वायु रक्षा प्रणाली जैसे रडार, कंट्रोल ऐंड कमांड सिस्टम (जो कि एयर स्पेस को कंट्रोल करते हैं) और वायुसेना बहुत मज़बूत हैं। यहां तक कि ड्रोन्स भी दुश्मन के ड्रोन को रोक सकते हैं।’
‘यहां उनका रोल मूल रूप से हवा में बहुत ऊंचाई पर उड़ान भर कर दुश्मन के विशेष क्षेत्रों पर नजऱ रखने और विशेष लक्ष्यों की जासूसी करने और अहम तस्वीरें लेने तक सीमित रहेगा।’
पिछले 8-10 वर्षों में युद्ध की प्रकृति बदल गई है और ड्रोन अब उनका एक अहम हिस्सा है। ड्रोन अब पारंपरिक युद्ध के बड़े प्लेटफॉर्मों जैसे टैंक व आर्टिलरी आदि को बहुत हद तक नुक़सान पहुंचा सकता है। इस पर दोनों देश काफ़ी ध्यान दे रहे हैं।
लेकिन राहुल बेदी मानते है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ड्रोन्स को लेकर रेस चल रही है।
उनके मुताबिक भविष्य में ‘रिमोट कंट्रोल वॉरफ़ेयर बढ़ेगा क्योंकि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी के साथ मशीन इंसान की जगह ले लेगी।’
वह कहते हैं कि दोनों परमाणु हथियार संपन्न देश हैं और अगर ग़लती से भी कोई ड्रोन किसी परमाणु संयंत्र के ऊपर आ गया तो गंभीर समस्या पैदा करेगा और इससे तनाव बढ़ जाएगा। (bbc.com/hindi)