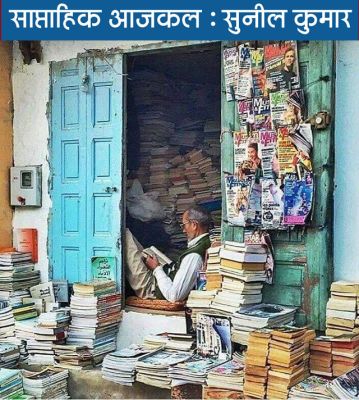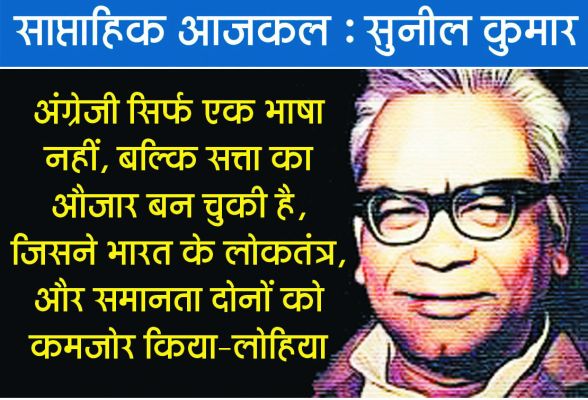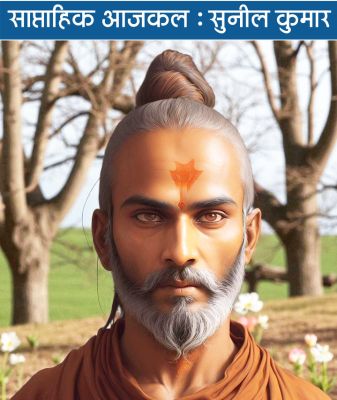आजकल

एक टीवी समाचार चैनल पर प्रस्तुतकर्ता-एंकर ने जब मेहमान-पैनलिस्ट से सवाल-जवाब किए, तो एक खास विचारधारा से आए हुए उस मेहमान ने अपनी विचारधारा के मुखिया के बारे में एंकर को कहा कि वे तो आपके भी अभिभावक हैं। इस पर एंकर ने साफ-साफ शब्दों में मना कर दिया, तो भी मेहमान अपने वैचारिक-मुखिया को एंकर का अभिभावक साबित करने में लगे रहे। मैंने यह पूरी बातचीत, या बहस देखी नहीं है, लेकिन कई गंभीर पत्रकारों की इस बहस पर पोस्ट देखी है, जो कि इस वैचारिक-असहमति को समझने के लिए काफी है। इस बात पर जाने का भी कोई अधिक मतलब नहीं रहता कि ऐसी बातचीत या बहस में आखिर में जीत किसकी हुई। यह कोई पंजा-कुश्ती, या सूमो-कुश्ती तो है नहीं जिसमें कि आखिर में किसी की जीत होना जरूरी हो, बल्कि कुछ मामलों में तो ऐसे मुकाबलों में भी टक्कर बराबरी पर छूट जाती है। वैचारिक विचार-विमर्श या बहस का बड़ा मकसद तो अलग-अलग विचारधाराओं और तर्कों को एक साथ सामने रखना होता है, ताकि देखने-सुनने वाले आगे उन पर अपना दिल-दिमाग लगा सकें। हर बातचीत किसी निष्कर्ष पर खत्म होने की उम्मीद करना एक बड़ा तंगनजरिया रहता है।
अब अगर बहस में शामिल कोई एक व्यक्ति अगर किसी को अपना अभिभावक मानना न चाहे, तो उसके धर्मांतरण की कोशिश क्यों करनी चाहिए? मैं अपने फेसबुक पेज पर लगातार अपने नास्तिक होने की बात लिखता हूं, और जहां-जहां मुझे नकारात्मक मिसालें मिलती हैं, मैं ईश्वर की धारणा, और धर्म के पाखंड के खिलाफ भी लिखता हूं। मेरे कुछ बहुत ही अच्छे और धर्मालु दोस्त ऐसे हैं जो मुझे अपने धर्म में ले जाने, या मुझे आस्तिक बनाने की कोशिश के बिना भी धर्म की अपनी समझ को लिखते हैं, और वह पढऩे लायक रहती है। दूसरी तरफ कई लोग इस जिद पर अड़ जाते हैं कि चूंकि मेरे माता-पिता आस्तिक थे, इसलिए मैं आस्तिक हूं, चूंकि मैं कुछ अच्छे काम भी करता हूं, इसलिए भी मैं धर्मालु भी हूं, और आस्तिक भी हूं। इस पर मुझे साफ करना पड़ता है कि मैं ईश्वर और धर्म नाम के झांसों से दूर हूं, और हाल-फिलहाल में किसी मौलाना या पादरी से मुलाकात का यह नतीजा नहीं है, स्कूली जिंदगी में ही अपने धर्मालु माता-पिता के बीच रहते हुए भी मैं ईश्वर और धर्म की हकीकत जान-समझकर अच्छा मजबूत नास्तिक बन गया था।
लेकिन मेरे नास्तिक रहने से परिवार के कुछ दूसरे लोगों के आस्तिक रहने का कोई टकराव नहीं है। जब तक पोप शंकराचार्य के धर्मांतरण की कोशिश न करें, और जब तक शंकराचार्य किसी बिशप को फिर से हिन्दू बनाने की कोशिश न करें, जब तक हिन्दूवादी लोग भारत की मुस्लिम आबादी को इस्लाम से परे करने पर न अड़े रहें, तब तक सहअस्तित्व में कोई दिक्कत नहीं है। अभी दो दिन पहले तो आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने साफ-साफ शब्दों में यह कहा है कि जो लोग भारत से इस्लाम खत्म करने की सोचते हैं, वे लोग हिन्दू नहीं हैं। उन्होंने साफ-साफ कहा कि भारत में इस्लाम पुरातन काल से रहा है, आज भी है, और भविष्य में भी रहेगा। यह विचार कि इस्लाम नहीं रहेगा, हिन्दू दर्शन नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में इस्लाम का हमेशा एक स्थान रहेगा।
भागवत की कही बातें पिछले बरसों से लगातार जलेबी की तरह सीधी रहती हैं, और उनके अगले बयान तक वे मीठी भी लगती रहती हैं। लेकिन आगे जाकर वे अपने ही बयानों से किनारा करने लगते हैं, और अभी-अभी वे 75 बरस की उम्र में रिटायर होने की चर्चा को खारिज कर चुके हैं, जो कि उनके ही एक बयान से अभी कुछ हफ्ते पहले जोर पकड़ रही थी। फिर भी हम अपने अखबार में भागवत के कहे हुए शब्दों को तब तक गंभीरता से लेते हैं, जब तक वे उसके उल्टे कोई बात नहीं करते। उनकी सबसे ताजा बात को हम उनकी सोच मानते हैं। बहुत से लोग हैं जिनका यह मानना है कि भागवत जो कहते हैं, और उस बात को साबित करने के लिए, या लागू करने के लिए उन्हें जो करना चाहिए, उसे वे करते नहीं हैं, महज कहते रहते हैं। ऐसे में अगर एक टीवी एंकर ने भागवत को अपना अभिभावक मानने से इंकार कर दिया, तो भागवत की विचारधारा के एक गंभीर और सीनियर आदमी को यह वल्दियत उस एंकर पर क्यों लादनी चाहिए? आज आल-औलाद ऐसी भी हैं जो अभिभावक का अपमान करती रहती हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं, जो किसी के अभिभावक न रहने पर भी उसका सम्मान करते हैं। वैचारिक असहमति किसी अपमान की वजह क्यों बने? और वैचारिक सहमति के लिए जिद क्यों करनी चाहिए?
मेरा तो हमेशा से यह मानना रहा है कि लोगों को वैचारिक असहमति के बीच रहने का हौसला रखना चाहिए क्योंकि असहमति को सुन-समझकर ही अपनी खुद की सोच को परिपक्व किया जा सकता है, वरना कीर्तन, प्रार्थना, और किसी दरगाह पर कव्वाली से कोई सोच विकसित नहीं हो सकती। लोगों के पास अपने मंच पर अपनी बात रखने का आज पूरा मौका रहता है क्योंकि सोशल मीडिया मुफ्त की आजाद जगह है। अपनी जगह पर आप कितनी असहमति, कितनी आलोचना, कितनी मोहब्बत, और कितनी नफरत को जगह देना चाहते हैं, यह भी आज फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म ने आसान कर दिया है। अब अखबारों में संपादक के नाम पत्र कॉलम में किसी शिकायत या विचार, या तारीफ के छपने के लिए संपादक की मर्जी जरूरी नहीं है, सोशल मीडिया पर आप अपनी बात को भरपूर तरीके से रख सकते हैं। ऐसे में एक टीवी एंकर ने यह दिलचस्प काम किया कि मेहमान प्रवक्ता के लादे गए अभिभावक को अपनी वल्दियत में लिखने से मना कर दिया। इस बात से और लोगों को भी सबक लेना चाहिए, शंकराचार्य को यह नहीं कहना चाहिए कि राम का नाम लो पोप, राम का नाम लो। और न पोप को चाहिए कि शंकराचार्य को बताए कि बपतिस्मा लेने के बाद यीशु सभी बीमारियां ठीक कर देंगे। लोगों को अपनी-अपनी दुकानों से अपने-अपने ब्राँड बेचने चाहिए। आपने कभी पावभाजी बेचने वाले को गुपचुप वाले के ठेले पर जाकर पावभाजी बेचते देखा है? दोनों के ग्राहक हैं, और दोनों एक-दूसरे के पीछे न लगें। और फिर, शंकराचार्य, और पोप के नामलेवा भक्तजन, दोनों ही मेरे सरीखे नास्तिक के पीछे न लगें।




.jpg)