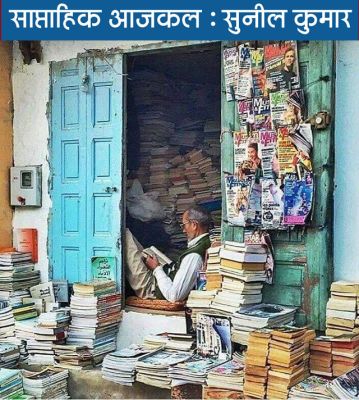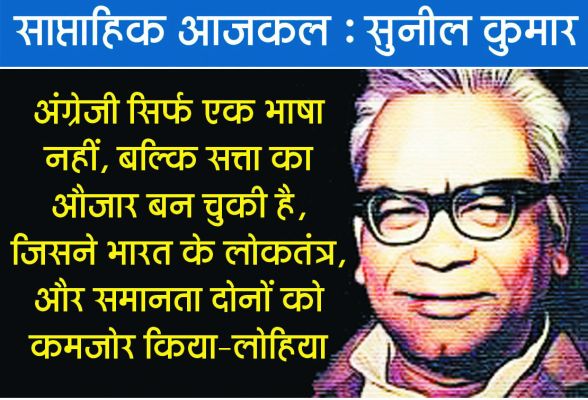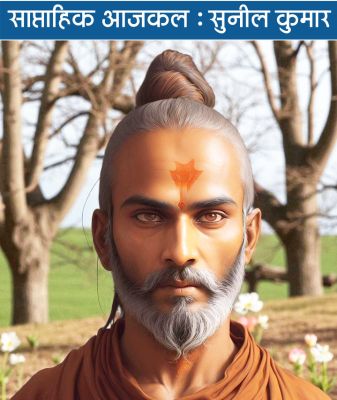आजकल
भारत में सूचना का अधिकार आए 20 बरस हो रहे हैं, और देश के साथ-साथ हर प्रदेशों में ये आयोग जनता को सूचना के अधिकार के तहत सरकारों से न मिलने वाली जानकारी को दिलाने के लिए बनाए गए हैं। जिस सोच के साथ यह अधिकार बना था, और यूपीए सरकार के समय कांग्रेस पार्टी के काबू के बाहर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी पर सीधा प्रभाव था, और उसी के चलते यह कानून बना था। बाद में हर पार्टी की सरकारों को यह समझ में आया कि यह तो सरकारों का भांडाफोड़ कर देने वाला कानून है, तो उसे कमजोर करने की तरह-तरह की राजनीतिक साजिशें शुरू हो गईं। अभी आई एक रिपोर्ट बताती है कि प्रदेशों के 29 आयोगों में लाखों शिकायतें पड़ी हुई हैं, और वहां सदस्यों की कुर्सियां खाली हैं, सरकारी विभागों से सूचना न मिलने के खिलाफ की गई अपीलें धूल खा रही हैं, और इस कानून का मकसद ही शिकस्त पा चुका है। इस क्षेत्र में काम करने वाले एक एनजीओ, सतर्क नागरिक संगठन ने आंकड़े सामने रखे हैं कि आज कुछ राज्यों में प्रदेश सूचना आयोग जिस रफ्तार से वहां आई अपीलों को निपटा रहा है, उस हिसाब से वहां आज की अपील पर फैसले में 29 बरस लग सकते हैं। तेलंगाना में 29, त्रिपुरा में 23, छत्तीसगढ़ में 11, एमपी और पंजाब में 7-7 साल लग सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और दो आयुक्तों के खाली पद अदालती स्थगन से नहीं भरे जा सके हैं, और इस स्थगन के पहले भी यहां की कुर्सियां खाली पड़ी थीं। आज इस छोटे से राज्य में 43 हजार मामले सूचना आयोग में पड़े हैं। अब तक आयोग ने जो आदेश दिए थे उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन पर आयोग ने सरकारी अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है, और ऐसी साढ़े 5 करोड़ की जुर्माना राशि भी आयोग तक अभी नहीं आई है। हैरानी की बात यह है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश में अभी जून के महीने तक कुल साढ़े 18 हजार आवेदन ही सूचना आयोग में थे, जो कि छत्तीसगढ़ के आधे से भी कम हैं।
जिन लोगों को सूचना आयोग की जरूरत और उसके असर का अंदाज नहीं है, उनके लिए यह बताना काम का होगा कि सरकारी विभागों से आमतौर पर भ्रष्टाचार और गड़बड़ी से जुड़ी जानकारी लोग आरटीआई में मांगते हैं, और विभाग की पूरी दिलचस्पी इसमें रहती है कि कोई जानकारी किसी तरह न दी जाए। कहावत-मुहावरे में सांप के किसी खजाने पर कुंडली मारकर बैठने की जो बात कही जाती है, वह सांप पर तो लागू नहीं होती, लेकिन सरकारी विभागों पर जरूर लागू होती है, जहां अधिकारियों का निजी, और वर्गहित इससे जुड़ा रहता है कि कोई जानकारी बाहर न चली जाए। सरकार में नीचे से लेकर ऊपर तक यही सोच रहती है कि आरटीआई को बेअसर कैसे किया जाए। यही वजह है कि कई-कई साल सूचना आयुक्तों की कुर्सियां खाली रखी जाती हैं। झारखंड में अभी पिछले बरस तक पांच साल से सूचना आयोग ठप्प पड़ा हुआ था। केन्द्रीय सूचना आयोग में भी नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के कई बार के आदेश के बाद हो पाईं।
लेकिन यह गिरावट सिर्फ सूचना के अधिकार के मामले में नहीं है, देश में और प्रदेशों में जितने तरह के संवैधानिक आयोग बनाए गए हैं, उन सबमें नियुक्तियां सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी की मर्जी से होती हैं, और फिर वहां मनोनीत लोग अपने को नियुक्त करने वाले लोगों के हित बचाने में लग जाते हैं। राज्य और केन्द्र के स्तर पर मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, बाल संरक्षण परिषद या आयोग, पर्यावरण से जुड़ी हुई संवैधानिक संस्थाएं, कॉलोनी और निर्माण से जुड़े हुए रेरा जैसे संवैधानिक संगठन, ऐसे बहुत से दफ्तर हैं जिन्हें बनाया तो इसलिए गया था कि वे सरकार में, या सरकार द्वारा किए गए गलत कामों पर नजर रखें, कार्रवाई करें, सरकारों को रोकें। लेकिन इनमें उन्हीं राज्यों की अदालतों या सरकारी विभागों से रिटायर होने वाले लोगों को भर दिया जाता है, या फिर सत्तारूढ़ पार्टी के पसंदीदा लोगों को। मतलब यह कि सरकार के बिठाए पिट्ठू मिट्ठू की तरह हाँ में हाँ मिलाते हैं, और जनता को मिलने वाला एक संवैधानिक हक मिलना शुरू होने के पहले ही खत्म होना शुरू हो जाता है।
मैं बरसों से इस बात को उठाते आ रहा हूं कि किसी भी राज्य के ऐसे किसी भी संवैधानिक आयोग में, या किसी नियामक संस्था में उस राज्य के लोगों को मनोनीत नहीं करना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक टैलेंट-पूल बनाना चाहिए, और कोई राज्य अपने संवैधानिक ओहदों के लिए उस पूल में से ही लोगों को छांट सके, या फिर केन्द्रीय स्तर पर बनाई गई एक संवैधानिक संस्था उसी तरह लोगों को किसी राज्य भेज सके, जिस तरह अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को केन्द्रीय स्तर से ही तय करके राज्यों में भेजा जाता है।
अब जब केन्द्र और राज्य सरकारों के सामने यह सहूलियत है कि वे बरसों तक संवैधानिक कुर्सियों को खाली रख सकती हैं, तो भला कौन सी सरकार अपने गलत कामों पर निगरानी की ताकत रखने वाली संस्थाओं को सक्रिय करना चाहेंगी? यह कुछ उसी तरह का होगा कि किसी शहर के चोरों को इकट्ठा करके कहा जाए कि वे श्रमदान से थाना बनाएं, और वहां पुलिस की तैनाती के लिए हर महीने आर्थिक योगदान भी दें। दरअसल सरकारों पर निगरानी के लिए बने संवैधानिक आयोग जब तक सरकारों की रहम पर चलेंगे, तब तक सरकारें उनका ऐसा ही हाल रखेंगी। आज तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्तियों, और उन्हें अलग-अलग राज्यों में भेजने के मामलों में केन्द्र सरकार जहां दखल दे सकती है, वह अपनी मर्जी से सब कुछ तय करवाने की कोशिश में लग जाती है। किसी भी सरकार से उसके पर कतरने वाली कैंची पर धार करने की उम्मीद बुनियादी रूप से एक गलत इंतजाम हैं। लोकतंत्र जैसी लचीली व्यवस्था में सरकारों से आदर्श की उम्मीद करना निहायत फिजूल बात है।
बात सूचना आयोग से शुरू जरूर हुई है, लेकिन वहां खत्म नहीं हो रही है। देश की अधिकतर संवैधानिक संस्थाओं की बदहाली देश में लोकतंत्र की बदहाली का एक जलता-सुलगता संकेत है। कोई भी लोकतंत्र उतना ही सफल हो सकता है जितनी सफल वहां की संवैधानिक संस्थाएं रहती हैं। भारत में जैसे-जैसे इन सारे आयोगों, और संसद की इमारतें मजबूत होती जा रही हैं, लोकतंत्र में इनकी एक-दूसरे पर निगरानी की ताकत उतनी ही कमजोर होती जा रही है। नाम के लिए ऐसी संस्थाओं को पालना जनता पर एक निहायत गैरजरूरी बोझ है। अब लोकपाल की ताजा मिसाल सामने है जिसमें धेले भर का काम न करने वाली इस संस्था के सात सदस्य 70-70 लाख रूपए की कार पाने जा रहे हैं। जनता को हक देने के लिए विकसित संवैधानिक सोच आज जनता का खून चूसने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)




.jpg)