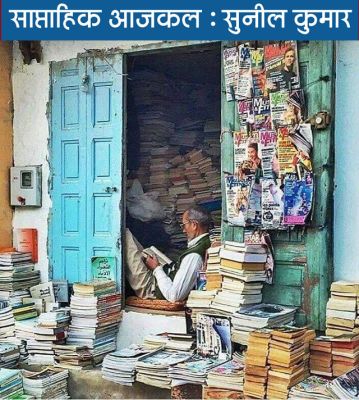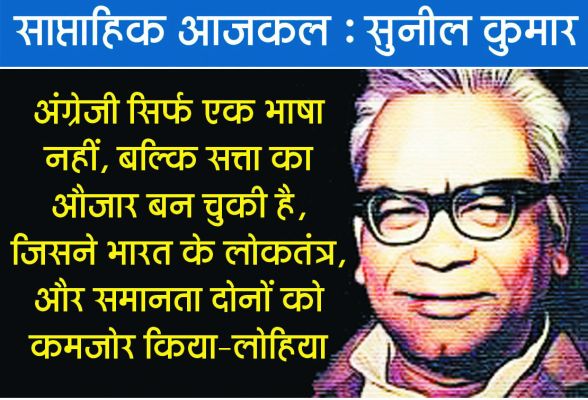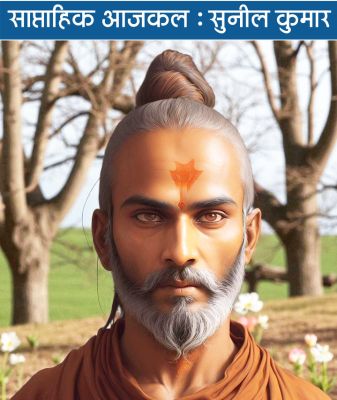आजकल

कुछ हफ्ते पहले देश के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की एसटी-एससी, और ओबीसी के लिए आरक्षित कुर्सियों की खबर आई थी कि इनमें से 80 फीसदी से अधिक खाली पड़ी हैं। अनुसूचित जनजाति के प्रोफेसर पद तो 83 फीसदी खाली हैं। इससे यह भी जाहिर होता है कि सरकार इन तबकों के लिए आरक्षित जितने पदों का यह मतलब निकालती है कि उन पर काम करने वाले लोग अपने बच्चों को भी आगे बढ़ा पा रहे होंगे, वह मतलब जायज नहीं है। दो बिल्कुल ही अलग-अलग खबरें और हैं जिन पर गौर करना चाहिए। एक खबर में कल ही राहुल गांधी ने यह कहा है कि देश की सबसे बड़ी निजी यूनिवर्सिटियों में दलित छात्रों का अनुपात एक फीसदी से कम है, आदिवासी छात्रों का अनुपात आधे फीसदी से भी कम है, और ओबीसी छात्रों का अनुपात 11 फीसदी है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े उनके नहीं है, बल्कि शिक्षा पर संसदीय स्थाई समिति के रिपोर्ट के हैं जिसने देश के चार निजी ‘इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस’ का सर्वे किया है। उन्होंने कहा कि संसदीय समिति ने यह साफ कहा है कि निजी शिक्षा में भी आरक्षण का कानून जरूरी है। इस बात से परे राहुल गांधी ने राजनीतिक बयान भी दिया है, लेकिन वह हमारी आज की इस चर्चा का मुद्दा नहीं है। एक अलग खबर और है, जिसे मैक्सेसे सम्मान प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडेय ने आज फेसबुक पर पोस्ट किया है। इस पोस्टर में सोशलिस्ट छात्रसंघ, और सोशलिस्ट युवजन सभा ने आंबेडकर, लोहिया, गांधी, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, ज्योतिबा फूले, जैसे लोगों की तस्वीरों के साथ यह मांग की है कि सिर्फ सरकारी विद्यालय में पढऩे वाले को ही सरकारी नौकरी मिले। समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए।
अब इन तीन बिल्कुल अलग-अलग बातों का आपस में कोई सीधा रिश्ता नहीं है, लेकिन इन तीनों का भारत की सामाजिक हकीकत से लेना-देना है जो कि इन तीनों बातों को बहुत तल्खी के साथ बताती है। मोदी सरकार ने जिन चार निजी विश्वविद्यालयों को ‘इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस’ का दर्जा दिया था, उसके पीछे बड़े-बड़े औद्योगिक घराने हैं। वहां दाखिला कितनी फीस पर होता है, वह एक अलग मुद्दा है, लेकिन उनके आंकड़ों को देखने के बाद अगर संसद की कमेटी निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के महत्व को दुहरा रही है, तो इस संसदीय समिति की सोच और भावना के साथ इन संस्थानों, और ऐसे दूसरे संस्थानों में दलित-आदिवासी, और ओबीसी छात्र-छात्राओं के अनुपात को देखना जरूरी है। ठीक उसी तरह जिस तरह कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की कुर्सियों पर एसटी-एससी और ओबीसी की गैरमौजूदगी समाज की बहुत ही कड़वी हकीकत बताती है। फिर ऊपर के पैराग्राफ में आखिरी बात समाजवादी-लोकतांत्रित सोच के छात्र और नौजवान संगठनों की उठाई हुई है कि सरकारी नौकरियां सिर्फ उन्हें मिलें जो सरकारी स्कूलों में पढक़र निकले हैं। जाहिर है कि निजी स्कूलों में महंगी शिक्षा पाकर निकलने वाले छात्र, बाद में महंगी कोचिंग पाकर हर किस्म की नौकरी पाने में आगे बढ़ जाते हैं, और गरीब बच्चे इन मुकाबलों में बराबरी के मैदान पर भी नहीं आ पाते। लोगों को याद होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने बरसों पहले यह फैसला भी दिया था कि सत्तारूढ़ नेताओं और अफसरों के बच्चों के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ें। जज की सोच यह थी कि सरकारी स्कूलों की खराब हालत सुधारने में ऐसा नियम मददगार हो सकता है कि सत्ता हांकने वाले लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, तो उनके मां-बाप की यह मजबूरी भी रहेगी कि वे इन स्कूलों को सुधारें। यह एक किस्म की समाजवादी सोच का फैसला था, जो कि लोकतांत्रिक-मानवीयता के हिसाब से अच्छा था, हालांकि हमने अपने अखबार में उसी समय यह लिखा था कि यह फैसला संवैधानिक रूप से सही नहीं है, और इस पर अमल नहीं हो सकेगा। वही हुआ भी।
आज देश में अधिकतर सत्तारूढ़ लोगों के बच्चे महंगे स्कूल-कॉलेज में पढ़ते हैं, और जो सचमुच ही अधिक तनख्वाह, या अधिक ऊपरी कमाई वाले लोग हैं, उनके बच्चे विदेशी विश्वविद्यालयों में पढऩे चले जाते हैं। ऐसे सत्तारूढ़ तबकों के बहुत से लोग देश के गरीब लडक़ों और नौजवानों को धार्मिक पाखंड में झोंककर और जोतकर रखते हैं क्योंकि उनके पास अच्छी तालीम पाने की कोई प्रेरणा नहीं रहती, और किसी तरह पढ़-लिखकर बेरोजगार बनने से उन्हें कुछ हासिल भी नहीं होता। धर्म और जाति के नाम पर इस पीढ़ी को सडक़ों पर उन्माद में झोंक दिया जाता है, और ऐसी भीड़ में अधिकतर लडक़े-युवक दलित-आदिवासी, और ओबीसी तबकों के ही रहते हैं। जिन तबकों को पढ़ाई में हर कदम पर आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए, वे धर्मान्धता में उलझा दिए गए हैं, जाहिर है कि ऊपर जाकर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से लेकर ऊंची पढ़ाई तक में उनकी कुर्सियां खाली हैं। कांवर से केन्द्रीय विश्वविद्यालय की प्रोफेसरी तक का सफर आसान तो हो नहीं सकता है। और अब ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को चुनावी घोषणापत्र में इस सामाजिक सच्चाई की जानकारी भी उम्मीदवारों से मांगकर मतदाताओं को देना चाहिए कि उम्मीदवार के बच्चे किन स्कूल-कॉलेजों में पढक़र किन विश्वविद्यालयों तक पहुंचे हैं, और अब क्या कर रहे हैं। इस जानकारी को पाकर हो सकता है कि ऐसे नेताओं के फतवों पर अपनी जवानी उन्मादी-कुर्बानी में झोंकने के बजाय लोग यह सोच सकेंगे कि नेताओं के बच्चे क्यों कांवड़ यात्रा में नहीं हैं, क्यों फौज में नहीं हैं।
धर्म और जाति ये दो ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन्हें छेडक़र पूरी की पूरी नौजवान पीढ़ी को सडक़ों पर लाया जा सकता है, उनके हाथों को किताबों और कम्प्यूटर से दूर करके, उनमें धार्मिक झंडे-डंडे थमाए जा सकते हैं, और उन्हें इस अफसोस या मलाल से स्थाई रूप से मुक्त रखा जा सकता है कि वे अच्छी पढ़ाई और अच्छी नौकरी क्यों नहीं पा सकते। आज की यह बात कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह विशुद्ध रूप से, और पूरी तरह एक सामाजिक मुद्दा है, और समाज के अलग-अलग तबकों को अपनी हकीकत, और अपनी जगह समझनी होगी। देश में जाति जनगणना के बाद यह सवाल और तल्खी से उठेगा, और इस जनगणना के सवालों में आदिवासियों को किधर गिना जाएगा, उन्हें अलग-अलग धर्मों में, या अलग-अलग जातियों में गिना जाएगा, या जैसा कि आदिवासियों के बीच से लंबे समय से यह मांग हो रही है कि उनके लिए एक सरना कोड लागू किया जाए, वैसा कुछ होगा?
इन तमाम बातों से परे यूपी के लखनऊ की एक खबर आई है जहां सरकार के किसी संपूर्ण समाधान दिवस शिविर में अफसरों के सामने एक बुजुर्ग महिला ने अपनी भयानक जिंदगी रखी, और बताया कि उसके पति का 25 साल पहले निधन हो गया, तो गांव के ही अशोक और अनमोल तिवारी घर आए, और उसके 10 साल के बेटे राममिलन को यह कहकर उठा ले गए कि उसके दादा ने तीन सौ रूपए उधार लिए थे, जिसे अपनी जिंदगी में उसका बेटा, यानी इस बच्चे का बाप अदा नहीं कर सका, इसलिए अब 10 साल का यह लडक़ा उनके पास मजदूरी करेगा। इस बूढ़ी महिला का कहना है कि 25 साल से उसके बेटे को बंधक बनाकर उससे मजदूरी करवाई जा रही है, और इस महिला को मरा हुआ दिखाकर उसका मकान बेच डाला, और अब परिवार की जमीन को भी हड़पने की तैयारी है। यह देश में एक सबसे ताकतवर मानी जाने वाली योगी सरकार के राज का हाल है।
इस देश के मीडिया से अधिक उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके मालिकाना हक से लेकर उसमें समाचार-विचार लिखने वाले, और उनके ऊपर के फैसले लेने वाले लोगों में एसटी-एससी, और ओबीसी गिनती के हैं। इसके लिए किसी जाति-जनगणना की जरूरत भी नहीं है, अखबारी पन्नों पर, और टीवी के समाचार बुलेटिनों में, मालिक, संपादक, लेखक-पत्रकार, और रिपोर्टर-एंकर के जितने नाम आते हैं, उन नामों को ही लिखते चलिए, और अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर उनके जात-धरम की गिनती कर लीजिए। फिर देश की आबादी में इन जात-धरमों का अनुपात देखकर हिसाब लगा लीजिए कि क्या विचारों के कारोबार में वंचित तबकों को कोई हक मिलता है? तो इस हिसाब-किताब के बाद आपका केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों के खाली पदों, और निजी विश्वविद्यालयों में एसटी-एससी, ओबीसी के अनुपात का दर्द जाता रहेगा। अधिक बुरा हाल देखकर उससे कुछ कम बुरा हाल भी अच्छा लगने लगता है, भारत में यही सामाजिक हकीकत है, लेकिन इसके ठीक-ठीक अहसास, और इससे आजादी पाने की भी जरूरत है। अगर सचमुच ही लोकतांत्रिक-न्याय की बात करें, तो इस सोच में क्या बुराई है कि सरकारी नौकरियां उन्हीं को मिलें जो सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं? (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)




.jpg)