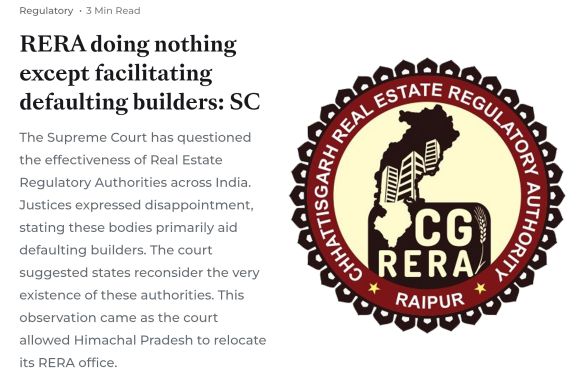संपादकीय

सोशल मीडिया राजनीतिक दलों के लोगों, और उनके खेमेबाज तथाकथित पत्रकारों के बयान लगातार ब्लॉक करने लायक रहते हैं क्योंकि राजनीति घटिया के जवाब में और अधिक घटिया होने के लिए बेसब्र, और उस पर उतारू रहती है। दूसरी तरफ खेमेबाज जर्नलिस्ट किसी नेता या पार्टी के हिमायती और ढिंढोरची एक्टिविस्ट की तरह काम करने, और उस शिनाख्त को अपने माथे पर सजाकर चलने में फख्र हासिल करते हैं। ऐसी खेमेबाजी के बीच किसी ईमानदार अखबारनवीस के लिए अपने को काबू में रखना, और अपने पेशे के साथ ईमानदार बने रहना किसी सुनामी में पैर जमाए रखने की तरह होता है, खासा मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन।
लेकिन जब बहुत से लोग चुनौती देने के अंदाज में हमारे अखबार को यह कहते हैं कि फलां ने इस जुबान में कहा या लिखा है, तो उसका जवाब तो इसी जुबान में हो सकता है, तो हम हाथ जोडक़र यह कहते हैं कि किसी भी तरफ की बदजुबानी में हमारी दिलचस्पी नहीं है। और यह बात सच भी है, जब गंदी जुबान के सैलाब, और गढ़ी गई तस्वीरों या वीडियो की आंधी आती है, और वह खासी बड़ी संख्या में पाठक और दर्शक दे जाती है, तो इस धंधे में बने रहने के बावजूद अपने पर काबू रखना कुछ मुश्किल लगता है क्योंकि आखिर जिंदा तो पाठकों या दर्शकों के बल पर ही रहा जा सकता है। यह भी समझने की जरूरत है कि आज जिस तरह की भाषा प्रचलन में आम और सर्वमान्य मान ली गई है, उसके बिना भी लिखते हुए, या बोलते हुए हमें कभी भाषा की किसी खूबी की कमी नहीं खली। अच्छी से अच्छी, और बुरी से बुरी बात बिना घटिया जुबान के कही जा सकती है। फिर हमें यह भी लगता है कि घटिया के मुकाबले घटिया जुबान या बातें बोलना, इससे तो जवाब देने वाले भी अपने आपको घटिया ही साबित करते हैं। आज भी सामान्य शिष्टाचार के दायरे में भी बड़ी-बड़ी बातें कही जा सकती हैं, तकरीबन हर बार।
सार्वजनिक जीवन के मुद्दों और लोगों पर लिखते हुए कई बार विशेषणों की जरूरत पड़ती है, और अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प जैसे व्यक्ति के बारे में लिखते हुए हम इसी संपादकीय कॉलम में जब बददिमाग, बेदिमाग, बदचलन, घटिया, तानाशाह जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें से कोई भी विशेषण नहीं रहता, वह इस घटिया आदमी के बारे में अदालतों में साबित हो चुका तथ्य ही रहता है। इसलिए जब किसी के बारे में इस्तेमाल किया जाने वाला आलोचना का विशेषण तथ्यों से साबित हो चुका रहता है, तो वह विशेषण भी नहीं रहता, महज तथ्य हो जाता है। हम अपनी आलोचना या तारीफ की भाषा को इसी सीमा के भीतर रखते हैं।
अब जब तारीफ की बात निकली है, तो सार्वजनिक रूप से किसी की तारीफ आलोचना की तरह ही होती है, जिसमें विशेषणों का तथ्यों से बड़ा ही कम लेना-देना होता है। किसी के गुजरने पर, या किसी के अभिनंदन के मौके पर, और बहुत से लोगों की जुबान में तो हर बरस आने वाली सालगिरह के मौके पर भी इतने विशेषण इस्तेमाल किए जाते हैं कि उन्हें पाने वाले को भी इस पर भरोसा नहीं होगा कि वे इतने अच्छे हैं। फिर भी किसी की झूठी तारीफ, चाहे वह मुसाहिबी की हद पार करती हो, किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं करती। लेकिन आजकल तारीफ से परे, किसी की आलोचना या निंदा में जिस जुबान का इस्तेमाल हो रहा है, वह तो लोकतांत्रिक, और मानवीय सीमाओं से बाहर-बाहर ही चलती दिखती है। ऐसी जुबान सिर्फ यही साबित करती है कि तथ्य और तर्क चुक चुके हैं, और इन विशेषणों के बाद अगली बारी नाली के कीचड़ की होगी। दिलचस्प यह भी है कि ऐसे कीचड़ के आकांक्षी पाठक और दर्शक बढ़ते चले जा रहे हैं, और कीचड़ के मुकाबले का जीवंत प्रसारण न करना मीडिया के धंधे में खासे घाटे का काम रहता है।
ऐसी तमाम नौबत के बावजूद अपने अखबार के लिए हमारा यह मानना रहता है कि अखबारों को अपने पुराने दिनों के तौर-तरीकों को याद रखना चाहिए जब वे मीडिया नहीं गिनाते थे, वे सिर्फ प्रेस कहलाते थे। उन दिनों सोशल मीडिया था नहीं, नतीजा यह होता था कि प्रेस को, यानी अखबारों को सोशल मीडिया सरीखे किसी प्लेटफॉर्म से प्रभावित होने की जरूरत नहीं रहती थी। अखबार प्रभावित होते नहीं थे, करते थे। और उनकी मौलिकता ही उनकी ताकत रहती थी जिसकी वजह से वे प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। इन दिनों कल के प्रेस कहे जाने वाले, और आज मीडिया में शुमार होने वाले अखबारों को सोशल मीडिया से प्रभावित होने से कोई परहेज नहीं है, और इसीलिए अब उनसे प्रभावित होने वाले लोगों, और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गिनती सीमित होने लगी है। जब सोशल मीडिया, जिस पर कोई संपादक नहीं है, की जुबान अखबार भी इस्तेमाल करने लगे, या संपादक और पत्रकार अपने सोशल मीडिया पेज पर उस जुबान में लिखने और बोलने लगें, तो फिर उनका असर सोशल मीडिया से अधिक कैसे हो सकता है? आज जब अखबार इस बात के लिए बेताब रहते हैं कि वे एक हरकारे या डाकिये की तरह ओछी जुबान में दिए गए एक बयान को दूसरों तक पहुंचाने के बाद उनसे इसका जवाब लेकर बाकियों तक पहुंचाने को अपनी गौरवशाली पत्रकारिता मानें, तो हम इस धंधे में पिछड़ जाना बेहतर समझते हैं।
आज टीवी समाचार चैनल जिस तरह सबसे घटिया बातों को, सबसे घटिया नजारों को बार-बार, बार-बार सुनाकर और दिखाकर टीआरपी बटोरते हैं, अगर उनसे सीखकर वही तरीका अखबारों को भी इस्तेमाल करना है, तो यह बेहतर ही होगा कि वे अपने आपको मीडिया ही कहें, और प्रेस न कहें। लोगों को यह याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर संपादक नाम की कोई संस्था नहीं है। और अखबार किसी संपादक के लिए शान या शर्म का सामान हुआ करते थे। आज जिन लोगों को शान और शर्म के बीच का फर्क नहीं रह गया है, वे अखबार को मीडिया का हिस्सा मानने के साथ-साथ, सोशल मीडिया का हिस्सा भी मान सकते हैं, और उसी अंदाज में छप सकते हैं। फिलहाल आज का यह लिखना सोशल मीडिया पर आज की घटिया बातों के संदर्भ में है कि उनके लिए वही एक बेहतर जगह है जहां कोई संपादक नहीं है। कोई भी जिम्मेदार और आत्मसम्मानी संपादक अपने अखबार को सोशल मीडिया की बदजुबानी से कुछ या अधिक हद तक अनछुआ रखने की कोशिश करते होंगे, ऐसी कम से कम हमारी उम्मीद तो है।