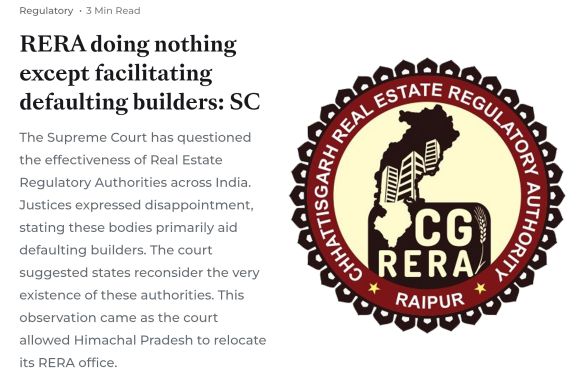संपादकीय

तस्वीर / अनिल लुंकड़
आज 9 अगस्त को दुनिया भर में विश्व मूलनिवासी दिवस मनाया जाता है। इसे भारत जैसे देश में विश्व आदिवासी दिवस भी कहते हैं चूंकि यहां आदिवासियों को मूलनिवासी मानने में कुछ राजनीतिक सोच आपत्ति करती हैं। फिर भी इसे अगर आदिवासी दिवस के रूप में भी देखें, तो भारत में सोचने के बहुत से मुद्दे हैं। हम किसी सरकार के कार्यकाल से जोडक़र इसे न देखें, और सिर्फ एक वैश्विक मुद्दे के रूप में देखें, तो दुनिया भर में तमाम जगहों पर आदिवासी उन्हीं जंगलों में बसे हुए हैं जिन पर शहरी कारोबारियों की नीयत है, पेड़ों की लकड़ी के लिए, उनके नीचे की खदानों में दबे हुए खनिजों के लिए, और जमीन या जल के लिए। जल, जंगल, और जमीन की यह लड़ाई उस वक्त और अधिक खूनी हो जाती है जब इसी जमीन के नीचे खनिज भी दबे रहते हैं। ये सब मिलाकर आदिवासियों को आज विश्व का सबसे नाजुक समुदाय बना देते हैं जिसकी बेदखली मानो होना तय है। कोई आदिवासी अपनी जमीन पर तभी तक रह पा रहे हैं, जब तक उसके ऊपर-नीचे, दाएं-बाएं कुदरत की दी गई इन नेमतों पर शहरी कारोबार और सरकार की नीयत नहीं आई है।
भारत में हम छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा जैसे बहुत से राज्यों के आदिवासियों को देखें, तो उन पर कई खतरे एक जैसे मंडरा रहे हैं। उनके बीच ईसाई संगठन उन्हें ईसाई बनाने में जुटे हुए हैं, और हिन्दू संगठन उन्हें ईसाई से हिन्दू बनाने में लगे हैं, और इन दोनों शहरी धर्मों में से किसी को यह बात मंजूर नहीं है कि वे आदिवासी थे, हैं, और बने रहें। आदिवासियों के सामने आज यह विकल्प नहीं छोड़ा गया है कि वे ईसाई या हिन्दू बने बिना अपने सांस्कृतिक-धर्म को मानते रहें। यह सिलसिला आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण के नारे के साथ एक ऐसी अजीब सी शहरी धर्मान्धता, और साम्प्रदायिकता को फैला चुका है कि इन दोनों धर्मों के पैदा होने के भी पहले से जो आदिवासी अपनी संस्कृति के तहत अपने ग्राम देवताओं के साथ जीते आए हैं, उन ग्राम देवताओं की कोई जगह भी अब नहीं छोड़ी जा रही है।
इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा मुद्दा आदिवासी समाज पर मंडरा रहा है, डी-लिस्टिंग का। जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं, उनका नाम आरक्षण से बाहर कर दिया जाए, यह मांग लेकर कई संगठन जगह-जगह आंदोलन कर रहे हैं, आज यह आंदोलन हिन्दू-राष्ट्रवादी संगठनों के हवाले है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इंदिरा गांधी के जीवनकाल में उनके कुछ सहयोगी भी यह आंदोलन उस समय चला चुके हैं। अब देश के आदिवासियों को आजादी के बाद की इस पौन सदी में संविधान के लागू होने के बाद के 70 बरसों में कुल एक यही चीज तो हासिल हुई है, और इस आरक्षण को भी धार्मिक आधार पर खत्म करने की मांग आज आक्रामकता के साथ की जा रही है। इस खतरे को समझने की जरूरत है कि आज अगर आदिवासी के ईसाई बनने पर आरक्षण खत्म किया जा सकता है, तो कल के दिन उनके हिन्दू बनने पर भी आरक्षण खत्म करने की बात आ सकती है। आज संविधान में उन्हें यह संरक्षण मिला हुआ है कि धर्म बदलने के बाद भी उनका आरक्षण का दर्जा बरकरार रहेगा, और इसी को खत्म करने का आंदोलन हिन्दूवादी ताकतें कर रही हैं। इस तरह जो हम बस्तर में देख रहे हैं, बाकी छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, आदिवासी समाज को रस्साकसी करने वाले ये दो धार्मिक समाज तरह-तरह से प्रभावित करने, बांटने, और डराकर रखने के काम में लगे हुए हैं।
दूसरी बात यह कि आदिवासियों की बेदखली करके जंगल और खदान की जमीन पर जो कब्जा देश भर में जारी है, उससे बचने का कोई जरिया आदिवासियों के पास नहीं है। उनके इलाकों में सामाजिक लीडरशिप नहीं पनप पाई, और सिर्फ बड़े राजनीतिक दल ही वहां पर दबदबा रखते हैं, और जैसा कि बड़ी पार्टियों का मिजाज होता है, वे बड़े कारखानेदारों के साथ हो लेते हैं। कभी-कभी किसी प्रदेश में बड़े राजनीतिक दल किसी कारखानेदार के खिलाफ भी लिखते हैं लेकिन यह बहुत ही अस्थाई दौर रहता है, और आगे-पीछे वे कभी राज्य तो कभी केन्द्र सरकार में, कारोबारी ताकतों के अघोषित भागीदार बन जाते हैं। इसमें आदिवासियों के अपने नेता भी रहते हैं, और आदिवासी इलाकों पर, पूरे प्रदेश पर राज करने वाले गैरआदिवासी नेता भी रहते हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस पर इस समाज को इस खतरे पर भी चर्चा करना चाहिए क्योंकि आदिवासियों की सबसे बड़ी बेदखली इस देश में खनिजों को लेकर ही होने वाली है। वे न सिर्फ अपनी जमीन खो बैठेंगे, अपने सिर पर से अपने जंगलों का साया खो बैठेंगे, बल्कि अपने इलाके से हटकर और कटकर वे अपनी संस्कृति भी खो बैठेंगे। खनिजों से आदिवासी इलाकों के पानी पर कैसा प्रदूषण होता है, यह देखने के लिए बस्तर में पानी में घुले हुए लोहे को देखना काफी है, उस लाल पानी से लोग नहा भी नहीं सकते, और सरकारें उम्मीद करती हैं कि वे उस पानी को पीकर जिंदा रहें।
शहरी कारोबारों के हमले से होने वाले बेदखली के बाद आदिवासी अपने बोलियों को खो रहे हैं, संस्कृति, आस्था के केन्द्र, अपनी कला, और संगीत को, सब कुछ को खो रहे हैं। एक बड़ी दिक्कत यह भी है कि ऐसे इलाकों में सक्रिय राजनीतिक ताकतें कोई सामाजिक चेतना की संभावना भी नहीं छोड़तीं। इंसान के बदन में दिमाग किसी को नहीं सुहाता, ईवीएम मशीन पर बटन दबाने वाली उंगली सबको सुहाती है। कारोबारी और राजनीतिक ताकतों को अगर ऐसी उंगली बिना दिमाग के मिल जाए, तो वे उसके मनमाने दाम देने तैयार हो जाएं।
इस मुद्दे पर इन गंभीर बातों को लिखने का हमारा मकसद यह है कि आज का यह दिन समारोह और जलसों का नहीं है, आदिवासी गीत-संगीत, और नृत्य से इसे सजाने का नहीं है, बल्कि आदिवासी जिंदगियों पर जो असल, और शहरों के थोपे हुए खतरे मंडरा रहे हैं, उन पर सोच-विचार का यह दिन है, और आदिवासी समाज या उनके शुभचिंतकों को यही करना चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)