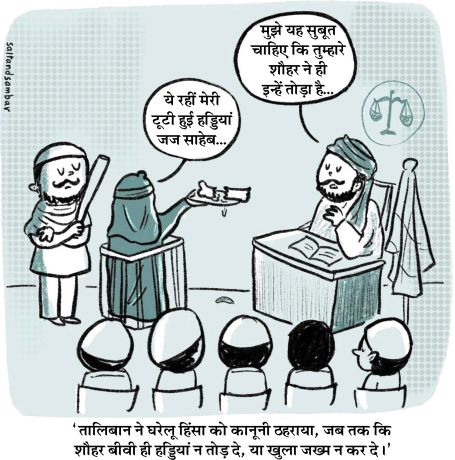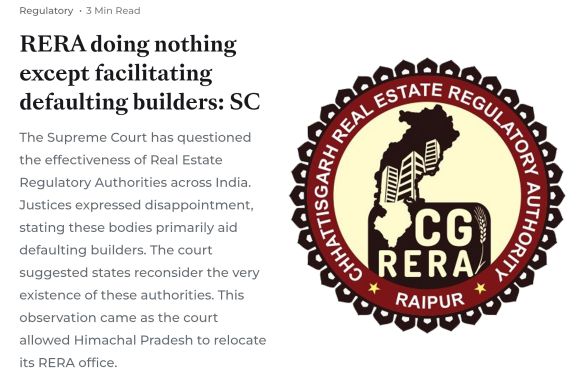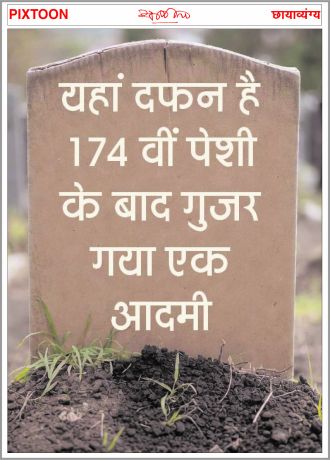संपादकीय

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक मामले पर दिए फैसले में कहा था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधानसभा से भेजे हुए विधेयकों पर एक निर्धारित समय में फैसला लेना चाहिए। अदालत ने यह भी तय किया था कि इन दोनों संवैधानिक पदों पर बैठे लोग किसी विधेयक को अंतहीन नहीं रोक सकते, और उन्हें जनता की चुनी हुई विधानसभा के फैसले का सम्मान करना चाहिए, और एक निर्धारित समय में उस पर अपना निर्णय दे देना चाहिए। दो जजों की बेंच ने जब यह फैसला लिखा था, तभी हमने कहा था कि केन्द्र सरकार इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका लगा सकती है, और आखिर में यह मामला एक बड़ी संविधानपीठ के सामने जा सकता है। अब राष्ट्रपति का पांच पन्ने का एक ‘संदर्भ’ सामने आया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए पूछा है कि क्या अदालती आदेश से राज्यपाल और राष्ट्रपति पर समय सीमा थोपी जा सकती है? उनके विवेक पर सवालिया निशान लगाकर प्रक्रिया तय की जा सकती है? राष्ट्रपति ने लिखा है कि संविधान ने जब ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं की है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है? राष्ट्रपति को आपत्ति इस बात पर भी है कि अदालत ने राष्ट्रपति के विवेक पर भी सवाल उठाए हैं? राष्ट्रपति का भेजा गया यह ‘संदर्भ’ सार्वजनिक रूप से सामने भी आया है, और उन्होंने कहा है कि इस फैसले से जितने तरह के सवाल उठ रहे हैं, वे सार्वजनिक महत्व के हैं, और उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय जानना जरूरी है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि संविधान ने राज्यपाल और राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा नहीं लगाई गई है। अब अदालत इस पर पांच जजों की एक संविधानपीठ बनाकर नए सिरे से गौर कर सकती है, और दो जजों के फैसले को दुबारा देख सकती है।
यह पूरा मामला बड़ा ही दिलचस्प इसलिए है कि यह संविधान की व्याख्या को लेकर बड़े बुनियादी सवाल खड़े करता है। और यह जाहिर ही था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की तरफ से, या उनकी तरफ से केन्द्र सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में फिर उठाएंगे। इन दोनों पदों के बारे में यह समझना जरूरी है कि राज्यपाल अपने राज्य में संविधान प्रमुख रहते हैं। उनकी मंजूरी के बिना विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित विधेयक भी लागू नहीं हो सकते, और राज्यपाल उन्हें बरसों तक तकिया बनाकर सो सकते हैं। तमिलनाडु सहित कई राज्यों में ऐसा हो भी रहा था। यहां पर यह समझना जरूरी है कि राजभवन एक संवैधानिक संस्था तो है, लेकिन राज्यपाल जजों की तरह नहीं है जो कि सरकार से अलग हों। राज्यपाल केन्द्र सरकार को रिपोर्ट करते हैं, केन्द्र सरकार के आदेश-निर्देश पर काम करते हैं, और भारत जैसी राजनीतिक व्यवस्था में अगर राज्य में केन्द्र की सत्तारूढ़ पार्टी को नापसंद सरकार है, तो राज्यपाल केन्द्र के एजेंट की तरह भी काम करते हैं। ऐसे में राज्यपाल के काम को संवैधानिक काम मानना निहायत पाखंड की बात है क्योंकि अनगिनत मामलों में अलग-अलग राज्यों के राज्यपाल केन्द्र की राजनीति खेलते आए हैं। अब राज्यपाल से जो मामले राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए बढ़ाए जाते हैं, उनमें राष्ट्रपति यही काम करते हैं, और वे केन्द्र सरकार की मर्जी के मुताबिक विधेयकों को ताक पर धर देते हैं, बिना किसी समय सीमा के। राष्ट्रपति के कामकाज को देखें तो यह साफ है कि वे एक रबर स्टॉम्प की तरह रहते हैं जो कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल, यानी केन्द्र सरकार की लिखित-अलिखित मर्जी से कागजों पर सील-ठप्पा लगाते चलते हैं। राष्ट्रपति का अपना कोई विवेक नहीं होता, और वे केन्द्र सरकार के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही काम करते हैं। ऐसे में राज्यों से आए हुए विधेयकों पर राष्ट्रपति के फैसले केन्द्र सरकार की राजनीतिक पसंद-नापसंद के मुताबिक ही रहते हैं।
जो लोग भारत के संविधान को एक मूढ़ दस्तावेज मानते हैं, वे ही यह व्याख्या कर सकते हैं कि संविधान ने राष्ट्रपति के लिए, और राज्यपाल के लिए भी फैसले लेने पर कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। संविधान शब्दों का घूरा नहीं है, वह एक जीवंत दस्तावेज है। और संविधान को समझने वाले लोग इस बात को जानते हैं, और यह बात बहुत बार लिखी जा चुकी है कि संविधान शब्दों के साथ-साथ उसकी भावना का भी दस्तावेज है। लैटर एंड स्पिरिट, इसका मतलब ही होता है कि शब्दों के साथ-साथ लोकतंत्र, और प्राकृतिक न्याय की एक भावना भी इस कागजी दस्तावेज से जुड़ी रहती है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक अदालत है, जिसका अधिकार, और जिसकी जिम्मेदारी संविधान की व्याख्या की भी है। इसलिए राष्ट्रपति का यह तर्क एकदम ही खोखला है कि संविधान में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, और इसलिए अदालत भी उन पर कोई समय सीमा नहीं लगा सकता। भारत का संविधान यहां के लोकतंत्र का एक दस्तावेज है, न कि किसी सनकी तानाशाह की मर्जी का गुलाम। इस संविधान के हर शब्द, इसकी हर बात का लोकतांत्रिक होना भी जरूरी है, इसकी ऐसी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती जो किसी भी व्यक्ति को, संवैधानिक संस्था या दफ्तर को तानाशाह अधिकार दे दे, जैसे कि वर्तमान राष्ट्रपति चाह रही हैं। यह अब कोई सामंतवादी व्यवस्था नहीं रह गई है जहां निर्वाचित विधानसभा राज्यपाल या राष्ट्रपति नाम के ओहदे पर बैठे हुए व्यक्तियों, और उनके पीछे पर्दे के पीछे छिपे हुए केन्द्र पर सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों, या गठबंधनों की जरखरीद गुलाम हो। यह बात शर्मनाक लग रही है कि राष्ट्रपति तानाशाह अधिकार पाने के लिए लड़ रही हैं, और लोकतंत्र को कुचलने वाला तर्क दे रही हैं। होना तो यह चाहिए था कि राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे हुए किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल और अपनी भूमिका को पूरी तरह से पारदर्शी, पूरी तरह से लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। राष्ट्रपति जो कि जनता की चुनी गई नहीं है, जिन्हें सांसदों, और विधायकों के बहुमत से चुना गया है, वे अपने को चुनने वाले विधायकों के फैसलों के खिलाफ एक तानाशाह की तरह बात कर रही हैं। हम मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एक व्यक्ति के रूप में आलोचना नहीं कर रहे क्योंकि उनका लिखा हुआ यह ‘संदर्भ’ (रिफरेंस) उनकी अपनी मर्जी का नहीं हो सकता, और इसे केन्द्र सरकार ने ही तैयार करके दस्तखत के लिए उनके सामने रखा होगा। केन्द्र पर सत्तारूढ़ किसी निर्वाचित सरकार को तो राज्य विधानसभाओं के अधिकार कुचलने की जरूरत और हसरत हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित विधानसभा के फैसले को बेमुद्दत कुचलने की हिमायती हो जाएं, यह बहुत ही खराब बात है। राष्ट्रपति को अगर किसी हक का बेमुद्दत इस्तेमाल करना था, तो उन्हें केन्द्र सरकार के तैयार किए गए इस ‘संदर्भ’ को ही बेमुद्दत रोककर रखना था। इससे और क्या होता, राष्ट्रपति को दूसरा कार्यकाल न मिलता! आखिर में हम एक बार फिर यह कहना चाहते हैं कि भारत का संविधान हजारों बरस पहले का कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है कि जिसके कोई शब्द बदले नहीं जा सकते। इस संविधान को अलग-अलग केन्द्र सरकारों ने सौ-पचास बार बदला हुआ है, संविधान की कई व्याख्याओं को पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया हुआ है, और वक्त-जरूरत के मुताबिक इसे हजार बार और भी बदला जा सकता है। राष्ट्रपति को तानाशाह बनने की हसरत नहीं पालनी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र को ऐसी कोई जरूरत नहीं है।