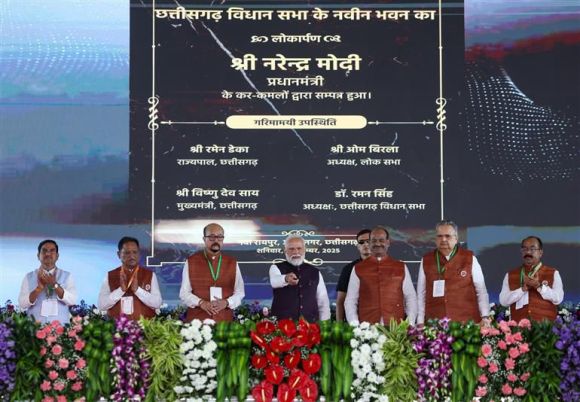संपादकीय

देश भर में पानी को लेकर एक सनसनी फैली हुई है कि इस गर्मी में पूरा देश ज्यादा तपने वाला है, और पानी की खूब कमी रहेगी। वैसे भी देश के कई हिस्सों में पानी नीचे जाते जा रहा है, और इससे दसियों करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। न सिर्फ शहरी इलाकों में, बल्कि गांवों में भी पानी का संकट इतना गहरा चुका है कि लोगों के लिए निस्तारी की मुश्किल हो रही है, और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से हर बरस भयानक तस्वीरें सामने आती हैं। जब इस नौबत में देश के मौसम के हाल को जोडक़र देखें तो लगता है कि एक तो जलवायु परिवर्तन का बुरा असर, दूसरा जमीन के नीचे के पानी का अंधाधुंध दोहन, इन दोनों बातों के चलते हुए हिन्दुस्तानी जिंदगी में बड़ा नुकसान आने जा रहा है। अभी गर्मी शुरू हुई भी नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कम से कम एक जिला मुख्यालय में यह आदेश निकल गया है कि नए भवन निर्माण की अनुमति अभी जल संकट को देखते हुए नहीं दी जाएगी। इसे अगर सिर्फ एक संकेत मानें, और आगे चलकर बाकी शहरों में, बाकी प्रदेशों में अगर जल संकट को देखते हुए भवन निर्माण रोके जाएंगे, तो उसका कितना व्यापक असर होगा यह सोचने की बात है। हर भवन निर्माण से दर्जनों से लेकर सैकड़ों तक मजदूर जुड़े रहते हैं, हुनरमंद कारीगरों का काम रहता है, भवन निर्माण सामग्री के ट्रांसपोर्ट में कारोबारी और उनके कर्मचारी लगे रहते हैं, मजदूर लगे रहते हैं, खदानें और ईंट भट्ठों का काम निर्माण से चलता है। अब अगर पानी की कमी से यह नौबत आने जा रही है, और यह नौबत अगर दूसरे कई इलाकों में पैदा होगी, तो क्या होगा? आज भवन निर्माण पानी की वजह से रूक रहा है, और दिल्ली जैसे शहर में भवन निर्माण ठंड के मौसम में प्रदूषण बहुत बढ़ जाने से रोका जाता है। तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन मजदूरों की जिंदगी पर कैसा असर पड़ेगा? जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी जितनी अधिक होने जा रही है, उससे इंसानों से परे जानवरों पर, कुदरत पर, और फसल पर भी बड़ा फर्क पडऩे जा रहा है। इस बारे में भी सोचने की जरूरत है।
लेकिन अभी हम सिर्फ गर्मी, और पानी की कमी के मुद्दे को जोडक़र अगर बात करें, और इंसानों के हाथ में इस नौबत को सुधारने के लिए क्या है, उस पर सोचें, तो यह साफ दिखता है कि पानी का अंधाधुंध नाजायज इस्तेमाल धरती के पेट को खाली कर दे रहा है। इंसानों को अपने अधिक ताकतवर पम्पों, और बिजली पर इतना भरोसा है कि वे हजार फीट की गहराई से भी पानी खींचकर निकालने पर आमादा हैं। इस बारे में राज्य सरकारों को एक नियम बनाना चाहिए कि जितने निजी ट्यूबवेल घरों में, या किसी कारोबार में लगे हुए हैं, उनमें से हर किसी पर मीटर लगाना चाहिए। आज पानी के इस्तेमाल का हाल यह है कि लोग प्रेशर पम्प की धार से कारों के चक्कों तक से धूल-मिट्टी धोते हैं, और फिर सडक़ से उस धूल-मिट्टी को हटाने के लिए पानी की धार का और इस्तेमाल करते हैं। लोग अपने घरों की छत पर कुदरत के खिलाफ जाकर बगीचे और लॉन लगाते हैं, और उनको सींचने के लिए अंधाधुंध पानी निकालते हैं। सरकारों के लिए यह फैसला कुछ कड़वा हो सकता है क्योंकि इससे संपन्न तबका नाराज होगा, लेकिन अगर धरती पर इंसानों को बचाना है, तो इतनी दूरदर्शिता अभी से दिखानी होगी कि पानी के इस्तेमाल पर टैक्स लगाया जाए। जमीन लोगों की मालिकाना हक की हो सकती है, लेकिन जमीन के नीचे के पानी पर उनका कोई निजी हक नहीं है। दूर-दूर तक बहने वाली भूगर्भ-जलधारा प्राकृतिक और सार्वजनिक सम्पत्ति है, और उसे पम्प के बाहुबल वाले संपन्न तबके की जरखरीद गुलाम नहीं बनाया जा सकता। सरकार को दिल कड़ा करके हर निजी ट्यूबवेल पर टैक्स लगाना चाहिए, और गर्मी के इन चार महीनों में कारों को पाईप की धार से धोने पर रोक लगानी चाहिए। छत्तीसगढ़ को बगल के विदर्भ के नागपुर से सबक लेना चाहिए जहां पर म्युनिसिपल ने पानी की पूरी सप्लाई का निजीकरण कर दिया, और दिन में दो-दो घंटे आने वाला पानी अब चौबीसों घंटे उपलब्ध है, गरीबों को एक सीमित मात्रा मुफ्त मिलती है जिससे उनका काम चल जाता है, और इससे अधिक खपत वाले लोगों को भुगतान करना पड़ता है। इसका नतीजा यह हुआ कि अब पानी के लिए सीमित घंटों में संघर्ष खत्म हो गया, और पानी की खपत भी कम हो गई। अब हर घर में टोंटी खोलते ही चौबीसों घंटे पानी है, और नागपुर शहर में नदी से आने वाले पानी की मात्रा भी कम कर दी गई है। हर चीज लोगों को मुफ्त देने से एक अलग किस्म की फिजूलखर्ची की आदत विकसित होती है। लोगों के दिमाग में यह बैठाने में कुछ हफ्तों की मेहनत लगेगी कि वे अपनी निजी जमीन के नीचे से मनमाना पानी नहीं ले सकते, और उन्हें मीटर के मुताबिक खपत का भुगतान करना पड़ेगा।
दूसरी बात यह कि शहरों में अब तक जहां-जहां सरकारी जमीनें खुली बच गई हैं, उनके इंच-इंच पर म्युनिसिपल और सरकार कुछ कमाऊ बना देना चाहती है। धरती को इतना घेरना तुरंत रोकना पड़ेगा, और शहरों में जितनी खाली जमीन है, उन्हें शहरी-जंगल लगाने में इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि शहरों का अधिकतम तापमान कुछ कम हो सके, और इंसान लू के इन महीनों में जिंदा रह सकें। गर्मी बहुत अधिक बढऩे से सेहत पर खर्च बढ़ रहा है, मजदूरी और कारोबार ठप्प हो रहे हैं, और पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।
फिर यह भी समझने की जरूरत है कि धरती के नीचे पानी आएगा कहां से? आज बारिश के महीनों में भारत के अधिकतर प्रदेशों में नदियों में बाढ़ आती है, और पानी समंदर में चले जाता है। हम कोई परमाणु रहस्य की बात नहीं कर रहे, यह मामूली समझ की बात है कि बारिश के अतिरिक्त पानी को नदियों में जाने से रोकना चाहिए ताकि वह पानी धरती के भीतर जल-भंडार को जिंदा रख सके, और बढ़ा सके। इससे नदियों में बाढ़ नहीं आएगी, समुद्र की सतह नहीं बढ़ेगी। आज हालत यह है कि धरती भीतर से खाली होती जा रही है, और समंदर में जल सतह इतनी बढ़ रही है कि दुनिया के बहुत से शहर उसमें डूबने जा रहे हैं। इन दोनों बातों का सीधा रिश्ता उन जगहों पर समझ में नहीं आता जो समंदर से दूर हैं, और जहां पर अभी तक पानी की कमी से हाहाकार नहीं मचा है। राज्य सरकारों को नदियों तक पहुंचने के पहले ही पानी को कैचमेंट एरिया में रोककर उससे बड़े-बड़े री-चार्जिंग तालाब बनाने चाहिए, और इस काम को गांवों के करीब करने, या मजदूरी देने जैसी सोच से भी परे रखना चाहिए। इसे सिर्फ धरती का जल-भंडार भरने के लिए किया जाना चाहिए, और जिन इलाकों से नदियों में पानी आता है, उन इलाकों में मशीनों से ऐसे बड़े-बड़े तालाब बनाकर उस पानी को धरती की गहराई तक जाने के लिए छोड़ देना चाहिए। आज दिक्कत यह है कि ऐसे किसी भी काम को मनरेगा जैसी मजदूरी की योजना से जोड़ दिया जाता है, या कि गांवों की निस्तारी के लिए तालाबों को उनके करीब बनाया जाता है। यह ध्यान रहे कि नदियों का कैचमेंट एरिया, और जमीन के नीचे पानी की धारा, इन दोनों का गांव और मजदूर से कोई लेना-देना नहीं रहता, और सरकारों को भूगर्भीय जल की जरूरत के लिए ऐसी बड़ी योजनाएं बनानी चाहिए। सरकार के पास नदियों तक पानी पहुंचने वाले इलाकों की शिनाख्त पहले से है, देश में खुदाई करने वाली बड़ी-बड़ी मशीनें चारों तरफ इस्तेमाल हो रही हैं, और बड़े-बड़े री-चार्ज तालाब बनाकर सरकार जलसंकट को आने वाले बरसों में खत्म कर सकती है।
इस मौसम पडऩे वाली अंधाधुंध गर्मी का हर इलाज आज की हमारी यहां की बातचीत में नहीं है, लेकिन हम उसके कुछ पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं जो कि सरकार, म्युनिसिपल, और नागरिकों के काम की हो सकती है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)












.jpg)