संपादकीय
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, सीएसई के एक कार्यकम में कल खुलासे से यह बताया गया कि राजधानी दिल्ली में यमुना के पानी में गंदगी मिलने के पीछे कौन सी वजहें हैं। इसका वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण देखकर यह हैरानी होती है कि जिन मामलों को दिल्ली में बैठी हुई राज्य और केंद्र सरकारें दोनों देखती हैं, स्थानीय म्युनिसिपलें भी जिसके लिए जिम्मेदार हैं, जहाँ का हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लगातार जिसे देखता है, उस यमुना का यह हाल कर रखा है। यह विश्लेषण बताता है कि किस तरह गंदे पानी को साफ़ करने के लिए लगाए गए एसटीपी कितने नाकाफ़ी हैं, और बिना साफ़ किया हुआ पाख़ानों और कारख़ानों का पानी सीधे यमुना में जाता है। कमोबेश इसी तरह का हाल देश के अधिकांश शहरों में है जहाँ पर निकलने वाले गंदे पानी के मुक़ाबले एसटीपी की क्षमता बहुत ही कम है। फिर यह सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी सरकारी प्लांट की घोषित क्षमता के मुक़ाबले उसका असली काम कितना कम होता होगा। दिल्ली जैसे शहर में यह भी हो रहा है कि इस तथाकथित साफ़ किए गए पानी को संयंत्र से निकालने के बाद फिर गंदे नालों से होते हुए यमुना में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। साफ किया पानी फिर गंदे नालों में ! देश की सबसे बड़ी आँखें जिस शहर-राज्य और उसकी नदी पर टिकी हुई है जब उसका यह हाल है, तो छत्तीसगढ़ में अगर गंदे पानी को साफ़ करने की घोषित सरकारी क्षमता भी ज़रूरत से बहुत कम है तो इससे किसी को सदमा नहीं लगना चाहिए।
यह भी समझने की ज़रूरत है कि देश की आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव चल रहा है, और ऐसे में देश के शहरीकरण को शुरू हुए और आगे बढ़े भी पौन सदी हो चुकी है। ऐसे में अगर अब तक शहर की साफ़ पानी की ज़रूरत, और उसी अनुपात में गंदे पानी की निकासी का अंदाज़ लगाकर पानी को साफ़ करने की क्षमता विकसित नहीं की गई है तो यह महज कल्पनाशीलता और योजना की कमी नहीं कहीं जा सकती, यह परले दर्जे की नालायकी भी है। यह उन नदियों के प्रति हिंदुस्तानियों की घटिया दर्जे की लापरवाही भी है जो कहने के लिए नदियों को माँ मानते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, और नदियों में डुबकी लगाकर अनगिनत त्योहार मनाते हैं। एक तरफ़ माँ कहना और दूसरी तरफ़ उसे गंदगी और जहर से पाट देना यह काम सबसे ग़ैर ज़िम्मेदार और अहसानफ़रामोश औलादें ही कर सकती हैं।
छत्तीसगढ़ में भी नदियों का प्रदूषण सिर चढ़कर बोलता है, कारखानों का प्रदूषण तो नदियों में मिल ही रहा है, शहर और गांव भी अपनी तमाम गंदगी तक़रीबन बिना साफ़ किए नदियों में छोड़ रहे हैं, जबकि सबसे आसान तरीका यह होता कि जिस दिन शहर-कस्बे की पानी की ज़रूरत का अंदाज़ लगाया जाता, उसके लिए योजना बनाई जाती, तो उसी योजना के एक दूसरे हिस्से की तरह गंदे पानी को साफ़ करने की क्षमता भी विकसित की जाती।
हिंदुस्तानियों ने निजी रूप से, और सार्वजनिक रूप से गंदगी में जीने की एक आदत डाल ली है। गंदगी के लिए जितना बर्दाश्त हमारे मिजाज में पनप चुका है, वह दुनिया के सभ्य देशों के लोगों को हैरान कर सकता है। जब गंदगी में रहने की नीयत हो, तब नियति भी वैसी हो जाना तय रहता है। हिंदुस्तान सड़कों पर, सरकारी इमारतों में, बाक़ी तमाम सार्वजनिक जगहों पर जितनी गंदगी करता है और उसमें जीता है, वह नदियों के साथ हमारे बर्ताव को भी तय करता है। इस देश में जिसको माँ माना जाता है उसको जिस तरह घूरों पर खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, उससे गंगा-यमुना माँ सरीखी नदियों के साथ हमारा बर्ताव भी तय होता है। हाल ही में हुए कुंभ में सबसे पवित्र समझी जाने वाली गंगा, और उसके सबसे अधिक पवित्र समझे जाने वाले त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं ने जिस दर्जे की गंदगी की है वह स्तब्ध कर देती है। लेकिन लोगों को अपनी श्रद्धा से अधिक महत्व किसी और चीज का नहीं लगता, श्रद्धा के केंद्र को साफ़ रखना भी महत्वपूर्ण नहीं लगता। बात सिर्फ़ जनता के सफ़ाई रखने की नहीं है क्योंकि शहरीकरण से जुड़ी गंदगी का इलाज निकालना सरकारों के ही बस का है, और जनता व्यक्तिगत हैसियत से इस बड़े काम को अपने स्तर पर पूरा नहीं कर सकती। शहरों में पानी की सरकारी सप्लाई से परे भी पानी की बहुत बड़ी तादात निजी ट्यूबवेल से निकले हुए पानी की रहती है जिसका अंदाज भी सरकार के पास नहीं रहता। इसलिए सरकार को गंदे पानी के निपटारे की अपनी क्षमता, पानी सप्लाई की अपनी क्षमता से बहुत अधिक आंकनी चाहिए, और एसटीपी का इंतज़ाम उस हिसाब से करना चाहिए।
जो देश, और पूर्वोत्तर भारत के जो प्रदेश नदियों को माँ नहीं मानते हैं महज़ नदी मानते हैं, वहाँ के पारदर्शी और साफ़ पानी को देखकर गंगा मैया की आँखों में आँसू आते होंगे, और उन्हीं आँसुओं से गंगा सहित दूसरी नदियों में बाढ़ आती है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)







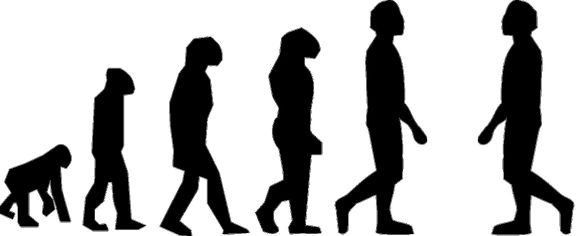




.jpg)

.jpg)


