संपादकीय

छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से एक है जहां सवा साल में चार चुनाव होते हैं। पहले विधानसभा का चुनाव, फिर लोकसभा का चुनाव, फिर नगरीय निकाय, यानी म्युनिसिपलों का चुनाव, और आखिर में पंचायतों का चुनाव। सरकार के बहुत से जरूरी फैसले नई सरकार आने, नए मंत्रियों में विभाग बंटने, फिर सरकार की पसंद के सचिव और दूसरे अफसर बदलने, नीतियों और कार्यक्रमों के बदलने से सरकारी कामकाज को लेट करते हैं। लेकिन जो काम सबसे अधिक प्रभावित होता है, वह है स्कूली शिक्षा का। मतदाता सूची नवीकरण से लेकर मतदान करवाने तक स्कूली शिक्षक भी झोंक दिए जाते हैं, और प्रदेश की हर सरकारी स्कूल मतदान केन्द्र तो बन ही जाती है। सरकारी शिक्षक किसी भी जिम्मेदारी से मना नहीं कर सकते, और नतीजा यह होता है कि हर पांच बरस में चुनावी साल एक ऐसा आता है जब सबसे कम पढ़ाई होती है, और बच्चों से उसी तरह इम्तिहान देने की उम्मीद की जाती है। इसमें तब दिक्कत और अधिक बढ़ जाती है जब किसी दूसरी पार्टी की सरकार आती है, और वह पाठ्यक्रम बदलने लगती है, या स्कूली इम्तिहान के तरीकों में फेरबदल करती है। यह आखिरी खतरा भी पांच साल में एक बार रहता है, और अगर सत्तारूढ़ पार्टी की निरंतरता बनी रहती है, तो ये तमाम दिक्कतें कुछ कम हो जाती हैं।
अब इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? मतदातासूचियों से लेकर मतदान केन्द्र और मतदान तक, मतगणना तक, प्रदेश में शिक्षक ही सबसे अधिक संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं, और स्कूली शिक्षा को एक ऐसा काम मान लिया जाता है जिसे जब चाहे तब रोक दिया जाए। कुछेक अदालती आदेशों के बावजूद स्कूली बच्चों को किसी जागरूकता रैली के बैनर थमाकर जब चाहे तब सडक़ों पर निकाल दिया जाता है। स्कूलों में इंतजाम, और स्कूली शिक्षा, यह किसी को ऐसी प्राथमिकता नहीं लगती कि उसमें बाधा रोकी जाए। सरकार के किसी भी काम के लिए जब जरूरत रहती है शिक्षकों से लेकर शाला भवनों तक, पढ़ाई के सारे इंतजाम को झोंक दिया जाता है। अभी म्युनिसिपल और पंचायत चुनावों में कई जगह हालत यह हो गई कि शाला भवनों में जहां मतदान केन्द्र बने थे, वहां पर एक-एक कमरे के बाहर पिछले तीन-तीन चुनावों के मतदान केन्द्रों के नंबर डले थे, और बोर्ड परीक्षा या किसी और इम्तिहान के लिए डाले गए कमरे के नंबर भी लिखे हुए थे। इन नंबरों से यह समझ नहीं पड़ रहा था कि इस चुनाव का बूथ क्रमांक कौन सा है। लेकिन यह नजारा यह भी बताता था कि इस चुनावी वर्ष में प्रदेश की स्कूलों में गैरशिक्षा कामों की कितनी दखल रही। हमेशा से शिक्षकों की यह शिकायत रही कि राज्य या केन्द्र सरकार के जितने तरह के सर्वे जैसे काम रहते हैं, उनमें शिक्षकों को गैरशिक्षकीय कामों में झोंक दिया जाता है, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है, और शिक्षकों का मनोबल भी टूटता है।
स्कूलों में पढ़ाई ठीक से हुए बिना अब इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, और हालत यह है कि स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, उनके शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए बाहरी लोगों को अनुबंध पर नियुक्त किया जाना ही अभी तक नहीं हो पाया है, और बच्चे बिना किसी शिक्षण-प्रशिक्षण के इस कोर्स का इम्तिहान देने जा रहे हैं। इसके अलावा इसी बरस नई सरकार ने 5वीं और 8वीं के इम्तिहान बोर्ड से लेना तय किया है। निजी स्कूलें इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गई हुई हैं, और वहां पर अभी सुनवाई चल रही है। इसके पीछे एक तर्क यह दिया जा रहा है कि शिक्षण सत्र के बीच में यह फैसला लिया गया, और स्कूलों में पढ़ाई बोर्ड परीक्षा के हिसाब से हुई ही नहीं है। इस बार चूंकि सरकार भी नई पार्टी की है, इसलिए परीक्षा प्रणाली और स्कूलों से जुड़ी दूसरी चीजों में कई फेरबदल भी हुए हैं, और इसलिए चुनावी वर्ष का असर बड़ा अधिक देखने मिल रहा है।
दुनिया में जो विकसित देश हैं, वहां पर जिन दो चीजों को समाज में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, उनमें से एक स्कूली शिक्षा है, और दूसरी चिकित्सा व्यवस्था रहती है। राज्य सरकार को ऐसे दीर्घकालीन नीति बनानी चाहिए जिसमें स्कूलों की पढ़ाई-लिखाई को लेकर न तो कोई बाधा आए, न उनमें तरह-तरह के प्रयोग किए जाएं, और न ही पढ़ाई के दिनों में किसी तरह की कटौती की जाए। राज्य सरकार को यह भी तय करना चाहिए कि छुट्टियों की अंतहीन लंबी लिस्ट को किस तरह स्कूली शिक्षा के लिए कम किया जा सकता है। कॉलेजों में तो पढ़ाई का बुरा हाल रहता है, और वहां माना जाता है कि झंडे से झंडे तक पढ़ाई होती है, यानी 15 अगस्त से 26 जनवरी के बीच। इसके आगे-पीछे का वक्त इम्तिहान, छुट्टियों, रिजल्ट, और दाखिले में निकल जाता है।
न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के हर प्रदेश में स्कूली शिक्षा को अधिक गंभीरता से लेने की जरूरत है, और दक्षिण के राज्य या महाराष्ट्र अपनी स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाकर ही अपनी अगली पीढ़ी को अधिक काबिल बना पाए हैं। जिन राज्यों में नौजवान पीढ़ी की यह बुनियाद ही कमजोर रह जाती है, वहां पर आगे की पढ़ाई में भी उन राज्यों के लोग बेहतर राज्यों की नई पीढ़ी का मुकाबला नहीं कर पाते। स्कूली शिक्षा नीति को राजनीतिक फैसलों से परे, और बड़े जानकार शिक्षाविदों के हिसाब से लिया जाना चाहिए।







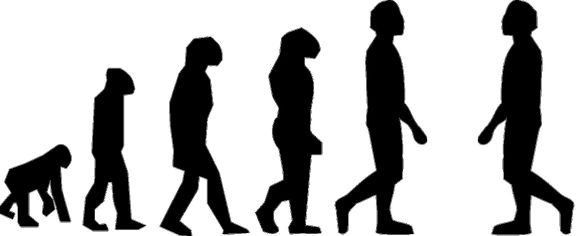




.jpg)

.jpg)


