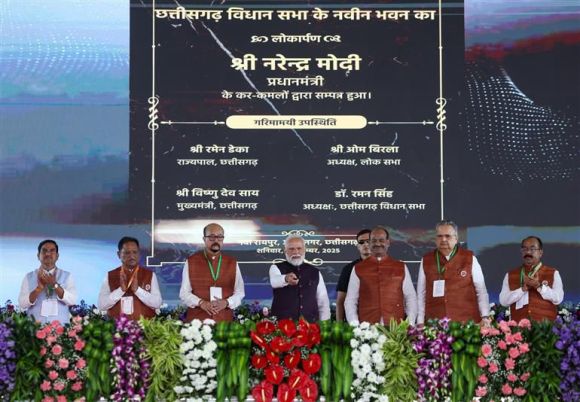संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह के मामले में यह फैसला दिया है कि अलग-अलग धर्मों के लोगों के लिए बनाए गए कोई भी पर्सनल कानून बाल विवाह जारी नहीं रख सकते। अदालत ने साफ किया कि पर्सनल कानून जो कि शादी, तलाक, विरासत जैसे मुद्दों के लिए अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग हैं, वे किसी भी तरह बाल विवाह का बचाव करने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अदालत ने केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए कई किस्म की सलाह भी दी है कि बाल विवाह रोकने के लिए उन्हें क्या-क्या करना चाहिए, और जरूरी हो तो एक कानून बनाकर बाल विवाह को गैरकानूनी करार देना चाहिए। हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हमने पिछले महीनों में लगातार इस बारे में अखबार या हमारे अखबार के यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल, पर लगातार इस बात को उठाया था, और लिखा था कि बच्चों के मानवाधिकार किसी भी धर्म के लिए बनाए गए कानून से ऊपर हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल यही फैसला दिया है, और हमारी लिखी और कही गई बात सही साबित हुई है। अभी एक बिल्कुल ताजा खबर यह थी कि भारत में 14 लाख से अधिक बच्चों पर बाल विवाह का खतरा मंडरा रहा है। यह आंकड़ा ऐसे समाजों के सर्वे पर आधारित था जो कि बाल विवाह के लिए जाने जाते हैं। देश भर में जगह-जगह सरकार के लोग बाल विवाह की खबर मिलते ही जाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, और परिवारों के सहमत न होने पर पुलिस कार्रवाई भी होती है। दो दिन पहले ही हमने यूट्यूब पर इस मुद्दे को उठाया था कि किस तरह पश्चिमी यूपी के बागपत में बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं, और वहां पर दो अलग-अलग मामलों में 15-15 बरस की बच्चियों ने सहायता केन्द्र फोन करके अफसरों को बुलाया, और अपनी शादी रूकवाई। एक लडक़ी के घर तो बारात भी पहुंच गई थी, और उसके बाद भी वह अड़ी रही। ये दोनों ही लड़कियां पढ़ाई करना चाहती थीं, और इसीलिए वे वक्त के पहले शादी के खिलाफ थीं।
सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर क्या रूख रहेगा, इसका अंदाज लगाना हमारे लिए अधिक मुश्किल नहीं था। सबसे बड़ी अदालत का रूख आमतौर पर प्राकृतिक न्याय के अनुकूल ही रहता है। समाज में प्राकृतिक न्याय अगर देखें तो लोगों के बुनियादी मानवाधिकार धार्मिक नियम-कायदों से ऊपर रहते हैं। इंसान तो धर्मों के बनने के दसियों हजार बरस पहले से चले आ रहे हैं जिस वक्त न कोई धर्म थे, न सामाजिक ढांचा था। उस वक्त भी अलग-अलग इंसानों के अलग-अलग अधिकार रहना ही प्राकृतिक न्याय था, यह एक अलग बात है कि उस वक्त न्याय की धारणा पनपी नहीं थी, और बाहुबल ही अकेला इंसाफ था। लेकिन तब से अब तक समाज व्यवस्था विकसित हुई है, और लोकतंत्र आने के बाद संविधान में लोगों के अधिकारों की अच्छी तरह व्याख्या हुई है। ऐसे में अलग-अलग धर्म या जातियों के लिए जो रीति-रिवाज को संरक्षण दिया गया है, उसे कभी भी लोगों के बुनियादी मानवाधिकार के ऊपर नहीं लादा जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मानवाधिकार की एक बड़ी बुनियादी समझ पर टिका हुआ है, और हमें यही उम्मीद भी थी कि यह अलग-अलग विवाह कानूनों के तकनीकी जाल में नहीं उलझेगा।
भारत में इसका सबसे बड़ा असर मुस्लिम समाज पर पड़ेगा जहां लड़कियों की माहवारी शुरू होते ही उन्हें शादी के लायक मान लिया जाता है। और 12-13 बरस की लडक़ी खुद तो कोई फैसला लेने लायक रहती नहीं है इसलिए मां-बाप उसे जिस खूंटे से चाहें, उससे बांध देते हैं। हैदराबाद जैसे शहर से भयानक खबरें आती हैं कि छोटी-छोटी बच्चियों को मरणासन्न बुजुर्गों के हाथों किस तरह निकाह के नाम पर बेच दिया जाता है, और ऐसे बूढ़े मर्द कुछ महीने एक नए बदन से खेलने के बाद उसे तलाक दे देते हैं, और ऐसी लड़कियां फिर अगली शादी के लिए कतार में खड़ी कर दी जाती हैं। हैदराबाद में ऐसे बाल विवाह रोकने के काम में लगे हुए एक संगठन ने एक मामला सामने रखा था जिसमें किशोरावस्था के पहले से शादी और तलाक झेलती हुई एक लडक़ी युवती बनने तक 18वीं शादी के लिए खड़ी कर दी गई थी। धर्म पर आधारित कोई भी समाज खुद होकर सुधरने को तैयार नहीं होता है, इसीलिए हिन्दू समाज में भी सतीप्रथा से लेकर देवदासी प्रथा तक कई चीजें बंद करवानी पड़ी थीं, और विधवा विवाह पर लगा हुआ सामाजिक प्रतिबंध खत्म करवाना पड़ा था। तकलीफ की बात यह भी है कि जितनी भी समाजों में इस किस्म की बुरी प्रथाएं चल रही हैं, वे अनिवार्य रूप से महिलाओं पर ही लादी जाती हैं, और मुस्लिम महिलाएं तो तीन तलाक का वार भी झेलती थीं जिन्हें मोदी सरकार ने एक कानून बनाकर गैरकानूनी करार दिया है, और अब ऐसे तलाकों पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने लगी हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ग्रामीण इलाकों में गरीब मजदूर परिवारों पर एक दबाव पड़ेगा जो कि पति-पत्नी दोनों के काम पर निकल जाने पर घर में अकेली लडक़ी छोडऩा नहीं चाहते। यह बात तो जाहिर है कि भारत में कहीं भी लडक़ी या महिला सुरक्षित नहीं हैं, ऐसे में गरीब परिवार लडक़ी की जल्द शादी करके उसकी जिम्मेदारी ससुराल पर डाल देते हैं। समाज के इस तबके को बाल विवाह के खिलाफ सहमत कराने में यह बात भी आड़े आएगी कि लडक़ी की हिफाजत की गारंटी कौन लेंगे? देश-प्रदेश की सरकारें तो इसमें पूरी तरह नाकामयाब साबित हो चुकी हैं, और जब बालिग हो चुकी लड़कियां और महिलाएं भी महफूज नहीं रह गई हैं, तब गरीब मजदूर परिवारों की बच्चियां किसके भरोसे सूने घरों में छोड़ी जा सकेंगी? इसके साथ-साथ आदिवासी समाज के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जिसके लिए अलग से कोई पर्सनल लॉ तो नहीं बना है, लेकिन समाज के रीति-रिवाज के मुताबिक इन्हें कई किस्म की छूट दी गई है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में बहुपति प्रथा जैसी बात को भी कानूनी माना गया है। इस आदिवासी समाज में कमउम्र में होने वाली शादियों का क्या होगा, इस बारे में भी केन्द्र और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के बाल विवाह के खिलाफ इस ताजा फैसले की रौशनी में कोई रास्ता निकालना होगा। कुल मिलाकर इस फैसले के बाद ही अब सरकारों पर, संसद और विधानसभाओं पर, और समाज पर भी दबाव पड़ेगा कि गैरकानूनी करार दिए गए बाल विवाह को पूरी तरह जड़ से कैसे मिटाया जाए।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)













.jpg)