संपादकीय

राज्यों की अर्थव्यवस्था को लेकर देश में कई तरह की फिक्र चलती रहती है, और हम भी उस बारे में लिखते रहते हैं। छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्य हैं जो कि खनिज से भरे-पूरे हैं, और लोहा, कोयला, सीमेंट पत्थर की मेहरबानी से राज्य को मोटी कमाई होती रहती है। कुछ राज्य पर्यटन की अर्थव्यवस्था पर चलते हैं, समंदर के किनारे के कुछ राज्य बंदरगाहों की वजह से माल के आयात-निर्यात का बड़ा फायदा पाते हैं, और तट पर ही कई तरह के उद्योग भी लग जाते हैं, गुजरात की संपन्नता की एक बड़ी वजह यह भी है। फिर बंदरगाह वाले राज्यों में ऐसे कारखाने भी अधिक लगते हैं, जो बाहर से आए हुए कच्चे माल से चलते हैं, या देश में ऐसे सामान बनाते हैं जो कि जहाजों से निर्यात हो जाते हैं। कश्मीर, राजस्थान, यूपी, और दक्षिण के कुछ राज्य बहुत समृद्ध हस्तशिल्प और हाथकरघा परंपराओं के कारोबार से भी संपन्न रहते हैं, और तीर्थ से लेकर दूसरे किस्म के पर्यटन तक का फायदा उन्हें देश-विदेश के सैलानियों की शक्ल में मिलता है। लेकिन ये तमाम चीजें कुदरत की वजह से मिली हुई हैं, किसी को खूबसूरत पहाडिय़ां मिली हैं, किसी को समुद्र तट मिले हैं, किसी को घने जंगलों में ऐसे वन्य प्राणी मिले हैं जिन्हें देखने दुनिया भर से लोग आते हैं।
लेकिन हम किसी राज्य की अर्थव्यवस्था, और उसमें किसी सरकार के योगदान का आंकलन इस हिसाब से भी करते हैं कि कुदरत की दी हुई चीजों से होने वाली कमाई से परे किस राज्य ने अपने इंसानों के हुनर और उनकी मेहनत से उनकी कमाई कितनी बढ़ाई है? खदानों से तो सरकार को कमाई होती ही है, लेकिन राज्य के नागरिकों की दक्षता और क्षमता को बढ़ाना, सिर्फ आम नागरिकों के बीच प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, सरकार की रियायत, और मनरेगा जैसे रोजगारों से परे सिर्फ नागरिकों की औसत आय को बढ़ाने का एक हिसाब राज्य सरकारों को लगाना चाहिए। अब अगर किसी राज्य में सोने या हीरे की खदान से कमाई शुरू हो जाए, या चलती हुई कमाई बढ़ जाए, वह एक अलग बात है। लेकिन अगर राज्य के कामगारों की औसत कमाई दस-बीस फीसदी भी बढ़ती है, और वह बाजार में मजदूरी या तनख्वाह में औसत बढ़ोत्तरी से अधिक बढ़ती है, तब हम उसे सरकार का योगदान मानते हैं। हमारा यह पैमाना थोड़ा सा जटिल इसलिए है कि देश-प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आंकड़े राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से लेकर राज्य के कारखानों तक की कमाई को आम मजदूरों की कमाई से जोडक़र औसत निकालने वाले रहते हैं। इन आंकड़ों से यह समझ नहीं पड़ता कि अपने नागरिकों को बेहतर रोजगार या कामकाज के लिए सरकार किस तरह तैयार कर रही है, या उनके लिए बेहतर मौके मुहैया करा रही है। किसी भी सरकार को अपनी उपलब्धि इस पैमाने पर अलग से आंकनी चाहिए कि उसने नागरिकों को कहां से कहां पहुंचाया है, और इसे आंकते हुए धान खरीदी जैसे काम पर भारी सरकारी अनुदान के आंकड़ों को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। आज खनिज रायल्टी की कमाई को अगर सरकार धान-किसान को दे देती है, तो इसमें सरकार ने जनता की कमाई में कोई स्वतंत्र बढ़ोत्तरी का योगदान नहीं दिया है।
हमारे ऐसे अलग पैमाने के पीछे हमारा एक मकसद है। इस देश में दक्षिण के तमाम राज्यों ने अपने लोगों को अंग्रेजी पढ़ाकर, टेक्नॉलॉजी सिखाकर, दुनिया भर की मशीनों पर काम करने के लायक उन्हें बनाकर उन्हें अधिक कमाई के लायक बना दिया है। आन्ध्र-तेलंगाना के लोग अमरीका में दसियों लाख की संख्या में काम कर रहे हैं, और अमरीकी पैमानों पर भी वे अधिक कमाई का काम कर रहे हैं। केरल के लोग खाड़ी के देशों में बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं, और वे केरल के अपने गांव-कस्बे या शहर में मुमकिन कमाई के मुकाबले कई गुना अधिक कमा रहे हैं। पंजाब के लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे बहुत से देशों में कामयाबी से बसे हुए हैं। हम राज्य के लोगों की क्षमता में उसी तरह की बढ़ोत्तरी देखना चाहते हैं ताकि वे अपने प्रदेश में उनके लिए मुमकिन कमाई से काफी अधिक कमाई का कोई काम दूसरे प्रदेश में जाकर कर सकें, या दूसरे देश तक भी जा सकें। आज यह बात साफ है कि सरकार की राशन-मदद, मनरेगा जैसी रोजगार योजनाओं, मुफ्त बिजली, महतारी वंदन जैसी अलग-अलग राज्यों की योजनाओं के चलते हुए, लोगों का भूखा मरना बंद हो गया है। लेकिन अगर आबादी का एक बड़ा हिस्सा महज इतने से संतुष्ट होकर बैठे रह जाए, तो उसका मतलब तो यही होगा कि उसकी क्षमता और संभावनाओं को बढ़ाने में राज्य का योगदान नहीं रहा। और साथ-साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य से मजदूर बाहर जाकर निर्माण कार्य करते हैं, ईंट भट्ठों पर ठेका-मजदूरी में घर के मुकाबले कुछ अधिक कमा लेते हैं, तो इसे हम राज्य की मानव क्षमता में विकास नहीं मानते।
आज दुनिया के कई देश गिरती हुई आबादी की वजह से परेशान हैं, और वहां पर बहुत बड़ी संख्या में कामगारों की जरूरत आज भी है, जो कि इस बाकी सदी में बढ़ती ही चलेगी। खुद चीन जैसा दुनिया का सबसे बड़ा कारखानेदार देश कामगारों की कमी से जूझ रहा है, और महज कागज पर संभावनाओं को देखें तो ऐसी भी संभावना बनती है कि भारत के मजदूर हुनरमंद हों, तो उन्हें चीनी कारखानों में भी काम मिल सकता है। यह सिर्फ एक काल्पनिक स्थिति है, क्योंकि दोनों देशों के बीच न अभी ऐसे रिश्ते हैं, और न ही सांस्कृतिक वातावरण ऐसा है। फिर भी आज हिन्दुस्तान के भीतर चीन के विकल्प के रूप में दुनिया की बहुत सी बड़ी कंपनियां अपना एक-एक कारखाना डालते चल रही हैं। इन कारखानों के लिए भी ऐसे ही राज्यों को छांटा जा रहा है जहां पर हुनरमंद कामगार हैं, और जो बंदरगाहों के करीब हैं। अब छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में बंदरगाह तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन सरकार अगर मेहनत करे तो यहां की नौजवान पीढ़ी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लायक ऐसा हुनरमंद बनाया जा सकता है कि वे सरकारी नौकरी के मोहताज न रहें। ऐसा किसी भी राज्य के लिए इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वहां से बाहर गए लोग अगर अधिक कमाते हैं, तो उसका एक हिस्सा अपने खुद के गांव-शहर में खर्च करते हैं, और वहां पर संपत्ति बनाते हैं जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान मिलता है। इसलिए देश के हर राज्य को अपने नौजवानों को काम दिलवाने के लिए अपनी सरहद के भीतर का तंग नजरिया नहीं रखना चाहिए, सरकारों को चाहिए कि नौकरी और रोजगार की अंतरराष्ट्रीय संभावनाओं को देखते हुए ऐसे नए कोर्स बनाएं जिन्हें करने वाले लोग अलग-अलग भाषाएं सीखकर उनके देशों में जाकर काम पा सकें। अपने लोगों को अगर सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए तैयार किया जाएगा, तो उनमें से भी 95 फीसदी लोगों को तो ये नौकरियां मिलेंगी नहीं, और वे राज्य पर ही बोझ बने बैठे रहेंगे। किसी नौजवान के बोझ बन जाने, और कमाऊ बन जाने के बीच का फर्क सरकार ही दूर कर सकती है। देश के भीतर भी जो विकसित राज्य हैं, वहां पर तो अब लगातार कामयाबी की वजह से सरकार से परे भी आम लोग और निजी क्षेत्र के स्कूल-कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर ऐसे रहते हैं कि वे नौजवान पीढ़ी को अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लायक तैयार कर देते हैं। हिन्दुस्तान के राज्यों को अपनी प्रति कामगार, गैर सरकारी अनुदान प्राप्त औसत आय का हिसाब लगाना चाहिए कि पांच बरस के कार्यकाल में लोगों को वह कहां से कहां तक पहुंचा पाई है।







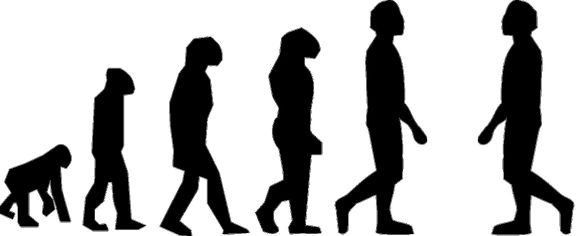




.jpg)

.jpg)


