संपादकीय
गुजरात में मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर अजान (आवाज लगाने) के खिलाफ लगाई गई एक याचिका को अहमदाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसे ध्वनि प्रदूषण बतलाते हुए, इसके शोर से परेशानी होने का तर्क देते हुए एक याचिकाकर्ता अदालत पहुंचा था, और अदालत ने इस याचिका को बुनियादी तौर पर गलत बताया, और वकील के तर्कों पर पूछा कि क्या दूसरे धर्मों की प्रथाओं से, जैसे मंदिर में पूजा या भजन के लिए संगीत बजाने से परेशानी नहीं होती? जज ने पूछा कि सुबह 3 बजे से ही ड्रम और संगीत के साथ मंदिरों में आरती होती है, क्या इससे शोर नहीं होता? अदालत ने यह भी पूछा कि क्या घंटे और घडिय़ाल का शोर सिर्फ मंदिर परिसर में रहता है, उसके बाहर नहीं जाता? यह याचिका बजरंगदल के एक नेता ने लगाई थी, और इस पर वहां के जज सुनीता अग्रवाल और अनिरुद्ध मेई ने यह भी याद दिलाया कि अजान तो दिन में अलग-अलग वक्त पर अधिकतम दस मिनटों के लिए होती है, और लाउडस्पीकर से एक इंसान की आवाज कितना ध्वनि प्रदूषण कर सकती है, वह जनता की सेहत के लिए कितना खतरा हो सकती है? हाईकोर्ट ने कहा कि हम इस जनहित याचिका को मंजूर नहीं कर रहे हैं। यह एक ऐसी आस्था है जिसका इस्तेमाल बरसों से किया जा रहा है, और यह कुल पांच-दस मिनटों के लिए होती है। उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा आपके मंदिर में सुबह तीन बजे से नगाड़ों और संगीत के साथ आरती शुरू होती है, क्या इससे किसी को तकलीफ नहीं होती? अदालत ने कहा कि इस याचिका का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, और ध्वनि प्रदूषण को नापकर उसके बाद बात करनी चाहिए थी।
जैसा कि जाहिर है कि मुस्लिमों के खिलाफ अतिसक्रिय संगठनों को मस्जिद की अजान से दिक्कत होती ही है। फिर चाहे दूसरे धर्मों के कई त्यौहारों पर रात-रात भर का रतजगा क्यों न होता हो? हिन्दुओं में अखंड रामायण का पाठ कई दिन क्यों न चलता हो? और मंदिरों के अलावा घरों में भी लाउडस्पीकर लगाकर कीर्तन करना या बजाना क्यों न चलता हो। यह तो भला हुआ कि बजरंगदल नेता अदालत गया, और कम से कम जजों ने इस बात को साफ किया है कि मस्जिदों की छोटी सी अजान की तुलना में मंदिरों के रात-दिन के लाउडस्पीकर की तुलना क्यों न की जाए? क्यों न इन दोनों किस्म के धार्मिक शोर को नापा जाए? हमारा ख्याल है कि सभी प्रदेशों और शहर-गांवों में ऐसा किया जाएगा, तो हिन्दुओं का उत्साह सबसे पहले ठंडा होगा जिनके धार्मिक लाउडस्पीकर कई बार तो कई-कई दिन बिना रूके चलते हैं।
अब हम गुजरात की इस खबर को एक बिल्कुल ही अलग खबर के साथ जोडक़र देखना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट पिछले कुछ बरसों से राज्य सरकार और जिला प्रशासनों को कटघरे में खड़ा करके चल रहा है कि धार्मिक और निजी जुलूसों में जिस अंदाज में अंधाधुंध ऊंचे शोरगुल के साथ डीजे (संगीत) बजता है, उस पर कैसे काबू किया जाए? वैसे तो हाईकोर्ट की अनगिनत चेतावनियों का अफसरों पर कोई भी असर नहीं हुआ है, लेकिन जब से इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य प्रशासनिक प्रमुख, मुख्य सचिव से एक के बाद एक कई हलफनामे लिए हैं, तब से जिला कलेक्टरों के हाथ-पांव थोड़े से हिले हैं, और अदालती हुक्म का हवाला देते हुए कलेक्टरों ने अपने मातहत अफसरों को हुक्म जारी किए हैं कि फलां-फलां कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाए। यह बात बड़ी दिलचस्प है कि कलेक्टरों के हुक्म में इन कानूनों के संबंधित पहलुओं का कोई खुलासा नहीं है, और हर थानेदार से उम्मीद की जा रही है कि वे अधिनियम को पढक़र उसे लागू करें। जो सामान्य समझबूझ से किया जाना चाहिए था, वह एकदम साफ-साफ और खुलासे वाला आदेश जारी करना था जिसे थानेदार के नीचे भी सिपाही तक समझ सके, लेकिन यहां थानेदार को किसी बड़े वकील की तरह मानकर सिर्फ अधिनियम का हवाला दे दिया गया है। और मजे की बात यह भी है कि कलेक्टरों के ऐसे आदेश में यह लिखा गया है कि स्कूल, अस्पताल, कोर्ट, या सरकारी दफ्तरों के सौ मीटर के दायरे में इस अधिनियम को लागू करें। अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ सरकारी महकमे के कान होते हैं? क्या निजी कारोबारियों, निजी दफ्तरों, सडक़ किनारे फुटपाथ पर ट्रैफिक का हर किस्म का प्रदूषण झेलकर काम करने वाले गरीब लोगों के कान नहीं होते? कलेक्टरों के आदेश में यह जिक्र भी किया गया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक वृद्धजनों, नि:शक्तजनों, और बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य और लोक शांति को ध्यान में रखते हुए ऐसे इलाकों को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि वृद्धजन तो किसी वृद्धाश्रम तक सीमित नहीं हैं, वे तो चारों तरफ बिखरे हुए हैं, वे घरों पर भी हैं, और बाजार में काम भी करते हैं, सडक़ किनारे मरम्मत करते हुए रोजी-रोटी भी कमाते हैं, इसलिए आबादी के किस हिस्से को इस दायरे के बाहर का माना जा सकता है? बीमार तो किसी भी इलाके के किसी भी परिवार के किसी भी उम्र के लोग हो सकते हैं, और जो बात अदालत के आदेश में नहीं भी आई होगी, वह साफ-साफ समझ में आती है कि छोटे बच्चों के नाजुक कानों पर ऐसे शोरगुल का बुरा असर पड़ता है, और सडक़ों पर जो जानवर पलते हैं, उनकी भी हालत खराब होती है। इस तकलीफ से परे, आज जब लोगों का बहुत सारा कारोबार फोन पर होता है, लोग इंटरनेट पर कई तरह की चीजें सुनकर पढ़ाई करते हैं, तो उन सबका नुकसान करना किसका हक माना जा सकता है?
अब सवाल यह उठता है कि क्या किसी राज्य की पुलिस को सिर्फ लाउडस्पीकरों को जब्त करने में झोंका जा सकता है? जब देश के कोलाहल कानून, और अदालतों या ट्रिब्यूनलों के आदेश में यह सीमा लिखी गई है कि किसी अहाते के बाहर दस डेसिबल से अधिक शोरगुल नहीं जाना चाहिए, तो फिर बहुत साफ-साफ आदेश निकालकर अदालत को ऐसे हर स्पीकर पर सीधी रोक लगा देनी चाहिए जिसकी आवाज दस फीट से दूर जाती हो? पुलिस के जिम्मे लाउडस्पीकरों की रोकथाम से अधिक जरूरी और भी कई चीजें हैं, और जब धार्मिक या किसी और किस्म की उन्मादी भीड़ कानून तोडऩे पर आमादा हों, तो गली-गली में पुलिस के साथ उनका ऐसा टकराव खड़ा करवाना ठीक नहीं है। अभी यह मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से पूरी तरह निपटा नहीं है इसलिए यह याद रखने की जरूरत है कि इसमें कुछ और व्यक्ति या जनसंगठन दखल देकर, या कि मौजूदा याचिकाकर्ता यह मांग कर सकते हैं कि ऐसे स्पीकर ही रोक दिए जाएं जिनका शोर दस फीट से दूर जाता हो। इसके अलावा जो अहाते लगातार कार्यक्रमों के लिए जाने जाते हैं, वहां पर हर कार्यक्रम के साथ में शोर नापने का इंतजाम होना चाहिए। यह मामला छोटा नहीं है। हमने आज के इस संपादकीय की शुरूआत तो गुजरात हाईकोर्ट से की है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक अलग किस्म की कोलाहल-हिंसा झेल रहा है, और उसा समाधान एक तर्कसंगत और न्यायसंगत अंत तक पहुंचाना जरूरी है।







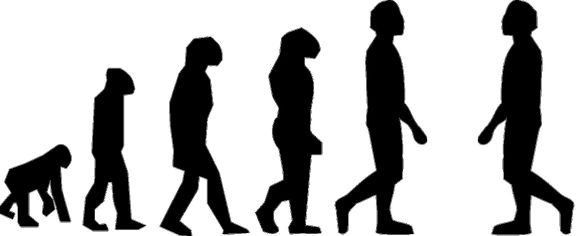




.jpg)

.jpg)


