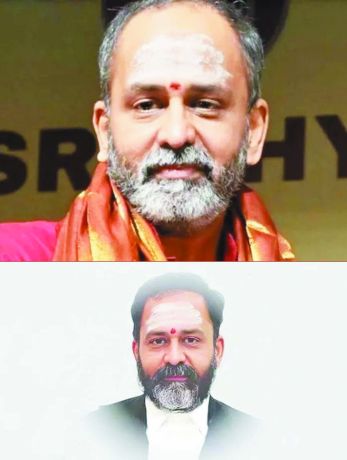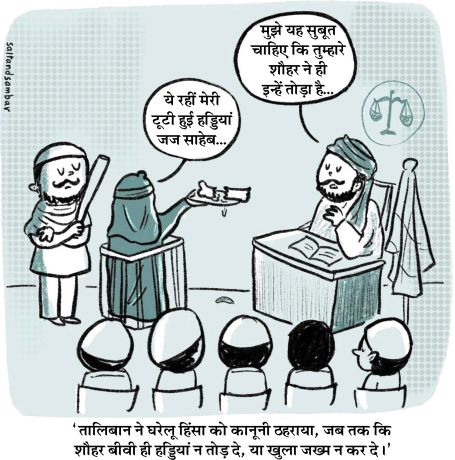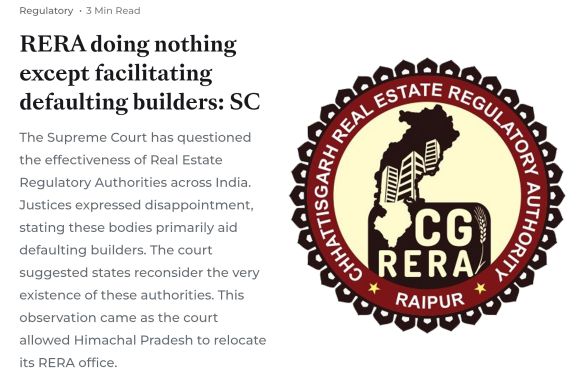संपादकीय
अब मानो कि हिन्दुस्तान में महंगाई, बेरोजगारी, मंदी जैसी सुबह से शाम तक की दिक्कतें खत्म हो चुकी हों, अब एक और बड़ा विवाद शुरू हुआ है। कल ही तमिलनाडु के शिक्षामंत्री का एक दीक्षांत समारोह में दिया गया भाषण टीवी पर छाया हुआ था जिसमें वे हिन्दी को पानीपूरी (गुपचुप) बेचने वालों की भाषा करार दे रहे थे, और अंग्रेजी पढऩे की वकालत कर रहे थे। आज वहां के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना को चि_ी लिखकर तमिल को मद्रास हाईकोर्ट की आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की है। उन्होंने इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय बेंच की भी मांग की है। कल जब दीक्षांत समारोह में हिन्दी के बारे में कुछ हल्की जुबान में मंत्री का भाषण हुआ तो देश की कुछ पार्टियों के नेताओं ने इसकी आलोचना की थी। अब मुख्यमंत्री ने जो मांग की है, उसमें हिन्दी के खिलाफ तो कुछ नहीं है लेकिन तमिल के हक की बात जरूर है। उन्होंने तर्क दिया है कि राजस्थान, एमपी, बिहार, और यूपी के हाईकोर्ट में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी भी आधिकारिक भाषा है, इसलिए हैरानी होती है कि अन्य राज्यों की राजभाषा को अंग्रेजी के साथ-साथ हाईकोर्ट की राजभाषा बनाने में क्या दिक्कत है?
इस मांग का एक दिलचस्प ताजा इतिहास अभी हफ्ते भर पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण है जिसमें उन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश और केन्द्रीय कानून मंत्री की मौजूदगी में कहा था कि देश भर में मौजूद अदालतों में स्थानीय भाषाओं में सुनवाई होनी चाहिए ताकि वहां के स्थानीय लोगों को कोर्ट की कार्रवाई और उसके काम करने के तरीके के बारे में समझ आ सके। मोदी का कहना शायद जिला अदालतों के बारे में था जहां आमतौर पर स्थानीय लोगों के मुकदमे चलते हैं, और स्थानीय भाषा जानने वाले वकील रहते हैं। अगर उनकी बात राज्यों के हाईकोर्ट के बारे में भी थी, तो भी यह बात समझ आती है क्योंकि जब अदालतों की भाषा लोगों की समझ से परे की रहती है तो उन पर वकीलों, जांच अधिकारियों, गवाहों, और कोर्ट कर्मचारियों के हाथों शोषण का खतरा मंडराने लगता है। वे यह भी नहीं समझ पाते कि उनके बारे में उनके वकील अदालत को क्या समझा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय भाषा को मजबूती देना, स्थानीय लोगों को मजबूत करना होगा। इसलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की यह मांग देश के हर हिस्से पर लागू हो सकती है, और अंग्रेजी के अलावा हिन्दी या उस प्रदेश की भाषा को अदालती भाषा बनाया जा सकता है।
आज देश के तमाम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी में काम करते हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी देश के अलग-अलग हिस्सों से आते हैं, और वहां वकालत करने वाले वकील भी गैरहिन्दी भाषी भी रहते हैं। ऐसे में बड़ी अदालतों की भाषा अंग्रेजी रखना एक सहूलियत की बात है क्योंकि तमिलनाडु से कोई जज उत्तराखंड जाकर वहां मामलों की हिन्दी सुनवाई शायद न समझ सकें। अगर भाषाओं की ऐसी व्यवस्था हाईकोर्ट में की जाती है, तो उससे फिर जजों के तबादलों पर भी एक किस्म की सीमा तय करनी होगी ताकि स्थानीय भाषा को समझने वाले जज ही वहां के हाईकोर्ट में तैनात किए जाएं। इसके बाद अदालती कार्रवाई, कागजात, आदेश और फैसले के अनुवाद का एक बड़ा काम शुरू हो जाएगा, और उसके बारे में भी सोचने की जरूरत पड़ेगी। आज तो किसी एक हाईकोर्ट की सुनवाई में दूसरे प्रदेशों की हाईकोर्ट के फैसले भी विस्तार से गिनाए जाते हैं, अलग-अलग प्रदेशों में क्षेत्रीय भाषाओं में काम होने से इस बारे में भी एक दिक्कत आ सकती है, लेकिन सभी दिक्कतों से पार पाने का भी रास्ता ढूंढा जा सकता है।
एम.के. स्टालिन ने जो दूसरा मुद्दा उठाया है वह सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय बेंच का है। यह बहुत नई मांग नहीं है, और दक्षिण के लिए इसकी मांग लंबे समय से होते आई है। दक्षिण के आधा दर्जन राज्यों के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट की ऐसी क्षेत्रीय बेंच बनती है, तो उससे दिल्ली पर बोझ भी घटेगा। लेकिन बड़ी संवैधानिक पीठ के लिए फिर भी मामलों को दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ेगा, और यह व्यवस्था किस तरह काम करेगी यह कानून-प्रशासन के बेहतर जानकार लोग बेहतर तरीके से बता सकेंगे। इतना जरूर है कि जब एक राज्य में हाईकोर्ट की अलग बेंच बन सकती है, तो देश में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बनाने की सोच में कोई खामी नहीं दिखती है, उस पर अमल के तरीके ढूंढने होंगे। तमिलनाडु की आज की सत्तारूढ़ द्रमुक पार्टी द्रविड़-अस्मिता के मुद्दे वाली पार्टी है, और भाषा से लेकर सुप्रीम कोर्ट के विकेन्द्रीकरण तक की बात उसकी विचारधारा से मेल खाने वाली उसकी पुरानी मांग है। आज देश की राजनीति और देश का वातावरण जिस तरह से हिन्दू, हिन्दुत्व, उत्तर भारत के मुद्दों से लद गया है, उसमें ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही है कि दक्षिण अपनी मौजूदगी भी दिखाना चाहे, और अपने हक का दावा भी करे।
हम पहले भी यह बात लिखते आए हैं कि दिल्ली के विकेन्द्रीकरण की जरूरत है। केन्द्र सरकार, संवैधानिक संस्थाएं, और विदेशी दूतावास, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जिस अनुपातहीन तरीके से दिल्ली में केन्द्रित हैं, वह तस्वीर बदलनी चाहिए। आज दिल्ली एक दमघोंटू शहर हो गया है, और इसे जीने लायक बनाने का तरीका यही है कि केन्द्र सरकार राज्यों से प्रस्ताव बुलवाए कि वे केन्द्र सरकार, और संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्रीय संगठनों के दफ्तरों के लिए अपने राज्य में जमीन या ढांचागत सुविधा, क्या दे सकते हैं। जिन दफ्तरों का एक-दूसरे से रोजाना वास्ता नहीं पड़ता है, उन्हें देश के अलग-अलग प्रदेशों में ले जाना चाहिए, इससे कामकाज का ढांचा तो बिखरेगा, लेकिन लोगों की आवाजाही से देश की एकता और अखंडता बढ़ेगी। आज हर बात के लिए दिल्ली की दौड़ लगाने से बेहतर यह होगा कि अलग-अलग दफ्तर अलग-अलग प्रदेशों में रहें ताकि वहां पर क्षेत्रीय विकास भी हो सके, और लोगों के बीच नकली राष्ट्रीयता के बजाय असली राष्ट्रीय एकता की भावना आ सके। ऐसा न होने का ही नतीजा है कि आज दक्षिण भारत अपने आपको उत्तर से कटा हुआ मानता है, उपेक्षित मानता है, और उसे यह लगता है कि राष्ट्रीय योजनाओं में उसे महत्व नहीं मिलता। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की कही बातों को भाषा और बेंच से परे भी भावना के स्तर पर समझने की जरूरत है, और फिर देश की शहरी योजना तो यह सुझाती ही है कि दिल्ली का विकेन्द्रीकरण किया जाए।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)