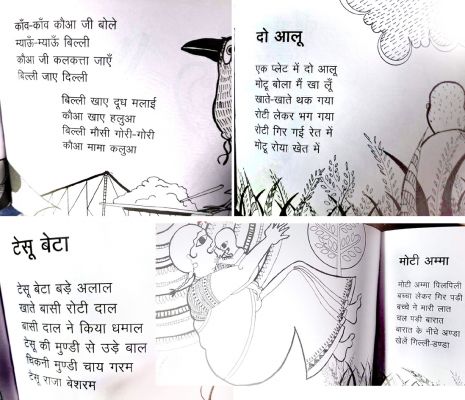संपादकीय
आज कांग्रेस पार्टी के भीतर चुनावी शिकस्त को लेकर दिख रही बेचैनी कोई नई बात नहीं है। दो बरस पहले जब पार्टी को लोकसभा चुनावों में उम्मीदों के खिलाफ जाकर बड़ी बुरी हार मिली थी तब भी यह बेचैनी शुरू हुई थी, और तब से अब तक जारी ही थी। लेकिन इसे पार्टी के खिलाफ गद्दारी भी कहा गया, लोगों की भाजपा में जाने की कोशिश भी करार दिया गया। लोगों को बार-बार यह नसीहत दी गई कि घर की बात घर के भीतर रखनी चाहिए, हालांकि यह बात किसी ने नहीं कही कि घर की बात घर के भीतर रखने के लिए उस घर तक आखिर पहुंचा कैसे जाए जहां पार्टी के नेताओं को भी महीनों और बरसों तक वक्त नहीं मिलता? खैर, कांग्रेस पार्टी की आज की बदहाली के बारे में अधिक चर्चा करना आज का मकसद नहीं है, बल्कि यह एक शुरुआत के लिए दिख रहा मुद्दा है जिस पर बात की जानी चाहिए।
किसी भी सरकार या संगठन के भीतर, या किसी कारोबार के भीतर भी अगर लोगों का आपस में सोचना-विचारना कम हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उनका आगे बढऩा भी बंद हो जाता है। जिस संगठन या कारोबार में ऊपर से फतवे आते हैं, और फिर वे नीचे के लोगों के लिए हुक्म बन जाते हैं, तो वहां पर गलतियों की सबसे अधिक गुंजाइश रहती है। गिनाने के लिए कई ऐसी मिसालें गिनाई जा सकती हैं कि फलां पार्टी तो एक व्यक्ति के हांके चलती आ रही है, और वह आगे भी बढ़ते जा रही है। लेकिन इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या वह सचमुच अपनी सभी संभावनाओं को पा सकी है? या फिर उन संभावनाओं से बहुत पीछे रह गई है, क्योंकि उसमें न तो कोई आत्ममंथन था, और न ही उसमें नई सोच, सोच की विविधता की कोई जगह रह गई थी। एक बंद टंकी के पानी की तरह उसकी सोच पर काई जमती चली गई, और ऐसी अधिकतर पार्टियां अपार संभावनाओं के रहते हुए भी एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पातीं या कांग्रेस की मिसाल अगर देखें तो आसमान की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद यह पार्टी नीचे मिट्टी में मिल गई है क्योंकि न इसमें सोच की विविधता की जगह रही, न सामूहिक नेतृत्व नाम की कोई बात रही। ऐसे में उसका यह हाल होना ही था। लेकिन राजनीतिक दलों से परे की भी बात करें तो सोच की विविधता, प्रतिभा का सम्मान, और खुला दिमाग रखना, इन सबकी वजह से कोई भी संगठन या कोई देश बहुत आगे बढ़ सकते हैं।
अब आज हिन्दुस्तान की एक सबसे बड़ी, और अच्छी-खासी साख वाली कंपनी टाटा को अगर देखें तो पारसी परिवार की शुरू की हुई कंपनी जिसके अधिकतर शेयर पारसी परिवारों के बीच थे, उसके अलग-अलग अफसर बदलते हुए आज एक दक्षिण भारतीय मुखिया इस कंपनी को चला रहा है। इसका न तो टाटा परिवार से कोई लेना-देना था, और न ही शेयर होल्डरों से। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनमें पेशेवर सीईओ काम करते हैं, और उसे आसमान तक ले जाते हैं। अमरीका में आज बड़ी-बड़ी कंपनियां चलाने वाले सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, इन्द्रा नूरी जैसे लोगों का उन कंपनियों से कोई लेना-देना नहीं था, वे केवल पेशेवर कर्मचारी थे, और कंपनियों के मुखिया बने। ऐसी कामयाब कंपनियों के भीतर यह बात रही कि लोगों के बीच साथ बैठकर सोचने-विचारने की आजादी रही। हिन्दुस्तान में आज कारोबार से लेकर सरकार तक, और राजनीतिक पार्टियों तक इसी बात की कमी है। जयललिता और मायावती जैसे लोगों के सामने दंडवत होना ही उनकी पार्टियों में विचार-विमर्श का पैमाना था। इनका अंत आगे-पीछे होना ही था। कुछ वैसा ही अंत अकाली दल का हुआ, समाजवादी पार्टी अपनी संभावनाओं तक नहीं पहुंच पाई, और लालू की पार्टी उनके कुनबे की गुलाम होकर खत्म हो गई। शरद पवार लंबे समय तक महाराष्ट्र के मुखिया रहने के बाद आज वहां के सत्तारूढ़ गठबंधन के तीन भागीदारों में से एक रह गए हैं, और केन्द्र की सत्ता में उनकी कोई भागीदारी नहीं रह गई है। इसलिए बदहाली हासिल करने वाली कांग्रेस अकेली पार्टी नहीं है।
दरअसल कामयाबी तक पहुंचने के लिए अपने घर के भीतर, संगठन के भीतर जिस तरह की आंतरिक असहमति का स्वागत होना चाहिए, वह जहां बिल्कुल नहीं रह जाता, वहां गलतियां ही गलतियां होने लगती हैं, और संभावनाएं धरी रह जाती हैं। संगठन या कारोबार के भीतर जहां असहमति का सम्मान होता है, वहां बहुत से दिमाग मिलकर काम करते हैं, वहां विविधता का फायदा मिलता है। लेकिन जहां असहमति को गद्दारी मान लिया जाता है, और विचार-विमर्श को बगावती तेवर करार दिया जाता है, वहां आगे बढऩा खत्म हो जाता है। हिन्दुस्तान में आज भाजपा जिस आसमान पर पहुंची हुई है उसके पीछे पिछले कुछ दशकों को देखें तो नेताओं की एक विविधता भी रही है। हर दो-चार बरस में पार्टी अध्यक्ष बदलते रहे, पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बदलते रहे, और वक्त आने पर लालकृष्ण अडवानी जैसे लोगों को हाशिए पर करके नई लीडरशिप आई, और उसने नई कामयाबी भी पाई। लोगों की आवाजाही जहां लगी नहीं रहती, वहां संगठन खत्म होने लगते हैं, आगे-पीछे यह खतरा ममता बैनर्जी की पार्टी के साथ भी रहेगा जहां वे अकेली ही सब कुछ हैं, और अगर उनके अलावा जरा सी गुंजाइश किसी और के लिए है, तो वह उनके भतीजे के लिए ही है।
सरकारों के भीतर भी यह देखने में आता है कि जहां प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपने फैसलों को लेकर किसी से सलाह-मशविरा करने के मोहताज नहीं रहते, वहां पर उनसे नोटबंदी जैसी ऐतिहासिक गलतियां होती हैं, और जिनसे उबरने की गुंजाइश हर किसी के पास नहीं होती, नरेन्द्र मोदी के पास तो फिर भी थी। इसके बजाय जिन सरकारों में सलाह-मशविरे की भागीदारी अधिक रहती है, उनमें कामयाब होने की संभावना भी अधिक होती है। सार्वजनिक जिंदगी से परे निजी जिंदगी में भी जो व्यक्ति या परिवार अपने बड़े फैसले अपने छोटे से दिमाग से अकेले लेते हैं, वे बड़ी गलतियां करने का खतरा अधिक उठाते हैं। इसलिए अपने आसपास के लोग, अपने संगठन या सरकार, या कारोबार के लोग न सिर्फ विचार-विमर्श के लिए साथ रखने चाहिए, बल्कि उन्हें उनकी असहमति को भी सामने रखने के लिए बढ़ावा देना चाहिए।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
भाजपा सरकार वाले कर्नाटक में सरकार द्वारा मुस्लिम स्कूली छात्राओं के हिजाब पर लगाई गई रोक को कर्नाटक हाईकोर्ट ने सही ठहराया है, और कहा है कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इस बारे में मुस्लिम छात्राओं ने याचिका लगाई थी जिसे खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल-कॉलेज में छात्र-छात्राएं यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। वहां जब से सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म से हिजाब पर बंदिश लगाई गई थी, बहुत से परंपरागत मुस्लिम परिवारों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था। अब समाज में इस प्रचलित व्यवस्था के चलते हुए इन लड़कियों की पढ़ाई का क्या होगा यह एक बड़ा सवाल इस अदालती फैसले के बाद खड़ा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल रहेगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के 9 जज इससे जुड़े हुए कुछ बुनियादी सवालों पर आखिरी फैसला नहीं लेते हैं, तब तक मुस्लिम लड़कियों को स्कूली पोशाक के साथ-साथ हिजाब की छूट दी जाए या नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई शुरू नहीं की है लेकिन हमारा यह मानना है कि हाईकोर्ट के फैसले के इस हिस्से पर तुरंत ही स्थगन देने की जरूरत है क्योंकि इससे मुस्लिम छात्राओं की पढ़ाई पर एक ऐसा नुकसान पडऩे वाला है जिसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। अगर परंपरागत समाज इस मुद्दे पर लड़कियों को स्कूल-कॉलेज भेजना बंद कर देता है तो वह भारत में लड़कियों की आत्मनिर्भरता के खिलाफ भी जाएगा।
अब कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले को अगर देखें तो इसमें संविधान की कुछ बुनियादी बातों को अनदेखा किया गया है। बहुत सी बातें संविधान की मूल धाराओं में लिखी हुई है जिनमें धार्मिक स्वतंत्रता, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी बातें हैं जिनमें पोशाक की पसंद भी शामिल है। यह फैसला ऐसी बातों का कोई न्यायसंगत निपटारा नहीं कर रहा है कि पोशाक की व्यक्तिगत पसंद और धार्मिक परंपरा का स्कूली पोशाक के साथ एक सहअस्तित्व भी हो सकता है। संविधान के जानकार लोगों ने इस फैसले को बहुत ही निराशाजनक और खामियों वाला माना है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस पर अमल तुरंत रोकने की उम्मीद भी की है। हम कानूनी बारीकियों के जानकार नहीं हैं, लेकिन प्राकृतिक न्याय की हमारी साधारण समझ यह सुझाती है कि धर्म के कट्टर प्रतीकों से परे भी धर्म के ऐसे प्रतीक हो सकते हैं जो लोग अपनी साधारण मान्यताओं के तहत मानना चाहते हैं, और इनमें हिजाब भी एक हो सकता है जो कि इस्लाम के तहत अनिवार्य चाहे न हो, वह इस्लाम को मानने वाले लोगों में एक धार्मिक परंपरा की तरह है। अब हिजाब या ऐसा कोई भी दूसरा प्रतीक किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा है, या उन धर्मावलंबियों के लिए वह एक प्रचलित परंपरा है, ऐसे महीन फर्क के बीच जब कर्नाटक हाईकोर्ट के जज फर्क करने बैठे हैं, तो उससे लोगों के बुनियादी हक खत्म हो रहे हैं। बाकी बहुत से धर्मों के बहुत से ऐसे प्रतीक हैं जिनका इस्तेमाल स्कूली पोशाक के साथ टकराव नहीं माना जाता। हिन्दू, सिक्ख, ईसाई धर्मों के कई प्रतीकों का इस्तेमाल छात्र-छात्राएं करते हैं, और उन पर एक हमलावर अंदाज में रोक अगर लगाई जाएगी, तो उससे इस देश में विविधता की बुनियादी खूबी खत्म होगी, और बहुत से तबके के लोगों को यह लगेगा कि देश में उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है।
कर्नाटक की भाजपा सरकार का शुरू किया गया यह बखेड़ा उसकी राजनीतिक ध्रुवीकरण की बदनीयत की एक हिंसक मिसाल है। उत्तरप्रदेश चुनाव के वक्त इसे शुरू किया गया था, और अब चुनाव के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी अपने बहुत ही तंगनजरिए की व्याख्या से सरकार और राजनीतिक ताकतों की इस कोशिश की आग में घी डालने का काम किया है। दिल्ली नेशनल लॉ स्कूल में संविधान पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर ने सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऐसे फैसलों को गिनाया है जिनको कर्नाटक हाईकोर्ट की इस बेंच ने अनदेखा किया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तब तक कानून रहते हैं जब तक संसद कोई नया कानून बनाकर उन्हें पलट न दे। ऐसे में हाईकोर्ट ने यह बहुत ही खराब और सामाजिक अन्याय का फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसलों को अनदेखा किया है।
अभी दरअसल सुप्रीम कोर्ट में धर्म के रीति-रिवाज को लेकर एक मामला चल रहा है, और संविधानपीठ उसकी सुनवाई कर रही है। इस मामले के बहुत से पहलू हैं, और उनमें से कुछ का अंतिम निपटारा होने तक कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले की अमल पर रोक लगानी चाहिए, और हिजाब की छूट दी जानी चाहिए। भारत के संविधान की बुनियादी समझ रखने वाले आम लोग भी यह बतला सकते हैं कि स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म का नियम साधारण धार्मिक परंपराओं को कुचले बिना लागू करने का एक आसान रास्ता जब है, तब एक अल्पसंख्यक तबके पर हमला करने की यह सरकारी सोच लोकतंत्र से बहुत परे की है। आज यह हमला सोच-समझकर मुस्लिम समुदाय पर हो रहा है, लेकिन बाकी धार्मिक अल्पसंख्यकों को यह समझ लेना चाहिए कि अगली बारी उनकी हो सकती है।
इस मुद्दे से जुड़ा हुआ एक दूसरा सामाजिक सवाल यह भी है कि क्या इस्लाम के तहत मुस्लिम समुदाय में पोशाक की हर तरह की बंदिश लड़कियों और महिलाओं पर ही लादने के इस सिलसिले को खत्म करना सारे देश की जिम्मेदारी नहीं है? आज जब किसी एक समाज को कुचलने की नीयत से कर्नाटक में यह सरकारी फैसला लागू किया गया है, तो उसे देखते हुए इस फैसले के समाज सुधारक होने का संदेह का लाभ देने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। फिर भी हम इस पहलू की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसे लादने वाले लोग इसे मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों का हिमायती फैसला बताने का तर्क भी दे सकते हैं, और वे कितने बड़े हिमायती हैं, यह बात उनके बाकी दर्जन भर फैसलों से और उनके हिंसक बर्ताव से आए दिन साबित होते रहती है। कुल मिलाकर कर्नाटक हाईकोर्ट का यह बहुत ही कमजोर और बेइंसाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते नहीं दिखता, लेकिन इस पर फैसला जल्द होना चाहिए क्योंकि जब तक इसे खारिज नहीं किया जाएगा तब तक एक तबके के बुनियादी अधिकार छिने रहेंगे।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
भारतीय रेल के मुसाफिरों को कोरोना लॉकडाऊन के पहले तक मिलने वाली टिकट पर रियायत अब शुरू नहीं की जा रही है। इसे लॉकडाऊन के बाद चलने वाली गिनी-चुनी रेलगाडिय़ों में बंद रखा गया था, लेकिन अब लोकसभा में रेलमंत्री ने यह जानकारी दी है कि रियायत पर यह पाबंदी जारी रहेगी। अब न तो लॉकडाऊन रहा, और न कोरोना की कोई लहर बची है, फिर भी बुजुर्ग मुसाफिरों को मिलने वाली यह बड़ी रियायत छीन ली गई है। ये लोग संख्या में कम हो सकते हैं, इनका सफर भी कम हो सकता है, लेकिन बुढ़ापे की सीमित कमाई या दूसरों का मोहताज रहते हुए सस्ती टिकट पर तो ये तीर्थयात्रा से लेकर रिश्तेदारी तक में आना-जाना कर लेते थे, अब टिकट रियायत में छूट खत्म होने से गरीब तबके के बुजुर्गों का तो मानो सफर बंद सा हो जाएगा, क्योंकि आज तो गरीबों के पास जवान लोगों के काम के लिए भी टिकट खरीदने की गुंजाइश नहीं बची है।
केन्द्र की मोदी सरकार ने हाल के बरसों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते हुए उन्हें 30-40 फीसदी से अधिक महंगा कर दिया है। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकटों को पांच रूपए से बढ़ाकर पचास रूपए कर दिया गया है। जहां-जहां रेलवे स्टेशनों का निजीकरण हुआ है वहां पर पार्किंग फीस भी कई गुना बढ़ चुकी है। महामारी से बचने के लिए और अपना खर्च बचाने के लिए रेलवे ने लॉकडाऊन के पूरे दौर में बिना रिजर्वेशन वाली टिकटें भी बंद कर दी थीं, और तरह-तरह की तरकीबें निकाली थीं कि सीमित मुसाफिरों की जेब से अधिक से अधिक पैसा कैसा निकाला जा सके। अब बुजुर्गों की टिकट पर जब रियायत खत्म की जा रही है तो कम से कम यह सोचा जाना चाहिए था कि महंगे दर्जे के डिब्बों में चाहे रियायत खत्म की गई होती, साधारण दर्जे पर तो इसे जारी रखना था। वैसे भी किसी भी सभ्य देश में बुजुर्ग नागरिकों का अलग से अधिक ध्यान रखा जाता है, और भारत में तो माता-पिता और बुजुर्गों की अतिरिक्त सम्मान की एक तथाकथित संस्कृति का दावा किया जाता है, जिसके चलते हुए भी इस तबके की जिंदगी से खुशी के ये पल छीन लिए गए हैं।
ऐसा लगता है कि चुनावों में लगातार जीत की वजह से केन्द्र सरकार की मुखिया भाजपा को अब देश के वोटरों के किसी छोटे तबके की फिक्र नहीं रह गई है। जब देश के लोग भावनात्मक मुद्दों पर रीझ कर वोट देने को आमादा हों, तो उन्हें किसी भी तरह की रियायत देने की जरूरत कहां रह जाती है? जब सौ रूपए लीटर पेट्रोल खरीदने वाले लोग मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए दो सौ रूपए लीटर का भी पेट्रोल खरीदने के फतवे देते रहते हैं, तो फिर उन्हें रियायत की भी क्या जरूरत है, और उनके टैक्स को भी असीमित बढ़ाने चलने में क्या दिक्कत है? अलग-अलग किस्म के सामानों को लेकर भारत की आम जनता पर बोझ हाल के बरसों में कितना बढ़ा है, इसकी एक लंबी फेहरिस्त बन सकती है। लेकिन जनता उससे भी बेफिकर है, और यही बात सरकार को असाधारण आत्मविश्वास देती है, उसे बददिमाग और बेरहम भी बना देती है।
दरअसल हिन्दुस्तान की तथाकथित जनचेतना का 21वीं सदी के किसी भी असल मुद्दे से सौतेला रिश्ता भी नहीं रह गया है। वह अधिकतर हिन्दुस्तान के इतिहास के एक हिस्से से लगातार जंग जारी रखे हुए है, और इसके लिए हिन्दुस्तान के इतिहास के एक दूसरे काल्पनिक हिस्से से हथियार भी निकालकर ले आती है, और आज की सत्ता को नापसंद इतिहास पर हमले करने लगती है। जब सारा का सारा आत्मगौरव ऐसे काल्पनिक इतिहास पर खड़ा होता है, तो उसे आज की पथरीली जमीन भला कहां सुहा सकती है। इस सिलसिले ने देश की जनता के रोजाना के दुख-दर्द को महत्वहीन बना दिया है। जब राष्ट्रवाद को भूख-प्यास से बढक़र महत्वपूर्ण बना दिया गया है, तो नोटबंदी की कतारों की तकलीफ, और लॉकडाऊन की घरवापिसी की तकलीफ की चर्चा होने पर लोग तुरंत कारगिल में छह महीने बर्फ में खड़े सैनिकों की तकलीफ गिनाने लगते हैं, और सवाल करने लगते हैं कि आम हिन्दुस्तानी की रोजाना की तकलीफें क्या उससे भी बढक़र हैं?
एक बड़ी दिक्कत यह भी हो गई है कि हिन्दुस्तानी जिंदगी में जिस तरह धर्म का महत्व बढ़ गया है, धर्मान्धता और साम्प्रदायिकता का महत्व बढ़ गया है, उसी तरह मीडिया और सोशल मीडिया का भी महत्व बढ़ गया है जो कि इस देश में सबसे अधिक हमलावर और दकियानूसी सोच से लदे हुए हैं। आज यह तुलना कर पाना मुश्किल है कि मीडिया अधिक पाखंडी है, या सोशल मीडिया। ऐसे में जिंदगी की सोच को चारों तरफ से घेरकर रखने वाले तमाम माध्यम इसी तरह के हो गए हैं। आज जब देश की सामूहिक जनचेतना कश्मीरी पंडितों की दिक्कतों को देखने, उन पर सोचने, और उन्हें सुलझाने के बजाय इस पर केन्द्रित है कि उन्हें कश्मीर से भगाने वाले लोगों का मजहब क्या था, और उस मजहब के लोगों को आज देश भर में किस तरह धिक्कारा जा सकता है, तो फिर बुजुर्गों की रेलटिकट-रियायत खत्म होने की क्या चर्चा करना?
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
होली के रंगों के बाद आज कामकाज शुरू होने को था कि पहली खबर ही बहुत खराब मिली। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के एक गांव में पेड़ पर एक नाबालिग जोड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लोगों का कहना है कि दोनों एक ही समुदाय के थे, और आपस में प्रेम करते थे, शादी करना चाहते थे, घरवालों की ओर से शादी की मंजूरी भी मिल चुकी थी, और इस बीच दोनों ने फांसी लगा ली। दोनों ही स्कूल में पढ़ते थे। इस मामले में फांसी कुछ अटपटी बात इसलिए लग रही है कि दोनों एक ही जाति के थे, और परिवार की तरफ से शादी की मंजूरी मिली हुई थी। आमतौर पर अलग-अलग जाति या धर्म के लडक़े-लड़कियों के बीच प्रेम होने पर परिवार और जात बिरादरी दुश्मन बन जाते हैं, और मोहब्बत की किस्मत दीवार में चुुन दी जाती है। ऐसे भी प्रेमीजोड़े की आत्महत्या हर कुछ दिनों में कहीं न कहीं होती है। हिन्दुस्तान में धर्म और जाति का, आर्थिक ताकत की अहंकार का, ओहदे के घमंड का हाल यह है कि मां-बाप अपने बच्चों की मौत बनकर सामने आते हैं, या बच्चे उनके हुक्म को अनसुना करें, तो वे अपनी तथाकथित इज्जत के लिए अपने हाथों अपनी औलादों को मार डालते हैं।
इस मामले के दो बिल्कुल अलग-अलग पहलू हैं, एक तो भारतीय समाज में प्रेम की संभावनाओं का, और दूसरा किसी भी तरह की वजह से आत्महत्या का। इन दोनों पर अलग-अलग गौर करना जरूरी है। जिस राजनांदगांव जिले से ऊपर की यह खबर आई है उसी जिले के एक दूसरे गांव में होली के दिन गर्भवती नवविवाहिता अपने मायके जाना चाहती थी, और पति को यह आपत्ति थी कि कुछ दिन पहले ही वह मायके से लौटी थी, इस पर बहस हुई, और पत्नी ने मिट्टी तेल छिडक़कर आग लगा ली, वह मर गई, और बचाते हुए पति झुलस गया। इस किस्म के घरेलू तनाव से आत्महत्या के भी बहुत से मामले सामने आते हैं। छत्तीसगढ़ में ही कल ही आत्महत्या की कुछ और खबरें भी आई हैं।
शहरीकरण के साथ-साथ जब अपने परिवारों से परे लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है, तो लोग अपनी मर्जी से शादी का हौसला भी जुटा पा रहे हैं। शादी के बिना भी प्रेम की संभावनाएं बढ़ती चल रही हैं क्योंकि पढ़ाई, खेलकूद, दूसरे तरह की गतिविधियों के चलते हुए लडक़े-लड़कियों को बाहर मिलने के मौके बहुत मिल रहे हैं, और उससे दोस्ती, प्रेम, और शादी की गुंजाइश भी बढ़ते चल रही है। इससे जाति व्यवस्था भी टूट रही है, और दकियानूसी समाजों में गोत्र को लेकर जो हिंसक जिद चली आती है, वह भी खत्म हो रही है। धर्मों के बीच भी अलगाव शहरीकरण की वजह से कम हो रहा है, और अंतरजातीय और अंतरधर्मीय शादियों से सामाजिक विभाजन भी घट रहा है। इसकी रफ्तार बहुत धीमी है, लेकिन यह सिलसिला शहरीकरण और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ आगे बढ़ रहा है। आज दिक्कत यह है कि हिन्दुस्तान की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा शहरों में नहीं है, और जो हिस्सा शहरों में है वह हिस्सा भी मां-बाप के काबू वाले समाज का अधिक है, इसलिए प्रेम विवाह के पहले हिंसा अधिक होने लगती है। ऐसे में निराश प्रेमी-प्रेमिका खुदकुशी पर उतारू हो जाते हैं क्योंकि पुलिस या समाज के बाकी लोग भी जाति व्यवस्था को कायम रखने पर आमादा रहते हैं।
प्रेम-संबंधों से परे भी हिन्दुस्तान में आत्महत्याओं के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। नेशनल क्राईम रिकॉडर््स ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ देश में आत्महत्याओं के मामले में तीसरे नंबर पर है, यहां पर हर बरस एक लाख आबादी पर 26.4 लोग खुदकुशी करते हैं, जो कि राष्ट्रीय आत्महत्या-औसत 11.3 प्रति लाख से ढाई गुना है। 2018 में छत्तीसगढ़ देश में पांचवें नंबर पर था, 2019 में चौथे नंबर पर आ गया, और 2020 में तीसरे नंबर पर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग-भिलाई, और रायपुर देश में आत्महत्याओं के मामले में देश में तीसरे और चौथे नंबर वाले शहर हैं। जिस प्रदेश में सरकार ने किसानों को इतनी सहूलियत दी हुई है वहां पर इतने लोग क्यों जान देते हैं, यह एक सामाजिक अध्ययन का विषय होना चाहिए। यहां पर इस वैज्ञानिक तथ्य को भी समझना जरूरी है कि कुछ आत्महत्याओं का कारण अनुवांशिकी भी होता है, अगर परिवार में पहले किसी ने खुद की जान ली है, तो इसका खतरा अधिक रहता है कि बाद में भी परिवार में कोई ऐसा करे।
आत्महत्याओं की रोकथाम की सामाजिक जागरूकता में लगे हुए लोगों ने यह पाया है कि इसकी बहुत सी बिल्कुल अलग-अलग वजहें हो सकती हैं। असफल प्रेम से लेकर इंटरनेट गेम्स से प्रोत्साहित होकर भी लोग खुदकुशी करते हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर पंजाब तक अलग-अलग बहुत से किसानी वाले राज्यों में किसानों की आत्महत्या हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, और देश में हरित क्रांति में सबसे अधिक योगदान देने वाले पंजाब में भी किसानों की आत्महत्या हर बरस सैकड़ों की संख्या में होती है, और इस आंकड़े को किसान आंदोलनकारी पूरी तरह फर्जी करार देते हैं। फिर भी देश के सरकारी आंकड़े पिछले कई बरसों से हर बरस दस हजार से अधिक किसानों की आत्महत्या दिखा रहे हैं। हिन्दुस्तान में असफल प्रेम या अवैध कहे जाने वाले संबंधों के तुरंत बाद किसानों की आत्महत्या के आंकड़े आते हैं। लेकिन समाज और परिवार को अपने बीच के लोगों की फिक्र करनी चाहिए जो कि तनाव से गुजर रहे हैं।
जानकार लोगों का यह मानना है कि आत्महत्या करने वाले लोग काफी सोचने-विचारने के बाद ऐसा करते हैं, और उनके व्यवहार से कई बार ऐसे संकेत मिलते हैं कि वे तनाव से गुजर रहे हैं, और उनका तनाव बढ़ते चल रहा है। कई बार उनके मुंह से निकलता है कि जिंदगी में क्या रखा है, कभी उनके बर्ताव में फर्क आ जाता है, कभी वे अपने चहेते सामान लोगों में बांट देते हैं, कभी किसी के सामने अपनी जिंदगी को बोझिल बताते हैं, कभी उनकी भूख गायब हो जाती है, या नींद खत्म हो जाती है, कभी वे अनजानी आवाजें सुनाई पडऩे की शिकायत करते हैं। ऐसी तमाम बातों पर आसपास के लोगों को नजर रखनी चाहिए, और उनका मानसिक उपचार करवाना चाहिए। इसके साथ-साथ परिवार और समाज के लोग, निराश लोगों के दायरे के लोग भी उनका हौसला बंधाने का काम कर सकते हैं। आज एक दिक्कत यह भी है हिन्दुस्तान में मानसिक इलाज की बात करने पर, या परामर्श के लिए ले जाने पर लोग उनके लिए लापरवाही और हिंसा से पागल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं।
आज हमारे इस अखबार सहित हर किस्म के मीडिया में आत्महत्या की खबरें रोज छपती हैं, और दुनिया भर के रिसर्च में यह पाया गया है कि आत्महत्याओं को बढ़ा-चढ़ाकर छापना या दिखाना, कई और लोगों को ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करता है। यही वजह है कि एक आत्महत्या की खबर कगार पर खड़े हुए कई दूसरे लोगों को भी वैसा करने के लिए प्रेरित करती हैं, या उन्हें उसका हौसला देती हैं। इसे नकल करते हुए की गई आत्महत्या कहते हैं। इसके ठीक उल्टे यह है कि अगर मीडिया में सकारात्मक खबरें आती हैं, ऐसी सच्ची कहानियां आती हैं कि कैसे लोग आत्महत्या की कगार पर पहुंचकर वापिस लौटे, और फिर जिंदगी में कामयाब हुए, तो उसके असर से कई संभावित आत्महत्याएं रूकती भी हैं।
इसलिए परिवार और समाज से लेकर मीडिया तक, सबको अपने-अपने किरदार को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है ताकि वे आत्महत्या को बढ़ावा देने के जिम्मेदार न बनें, और उसकी रोकथाम में मदद कर सकें।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभी दो जजों, प्रीतिंकर दिवाकर और आशुतोष श्रीवास्तव, की अदालत में एक वकील बिना गाऊन (लबादा) पहने पेश हुआ तो जजों ने उसकी आलोचना की, और इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि वे ऐसी हरकत पर बार काउंसिल को लिख सकते हैं लेकिन वकील के नौजवान होने की वजह से वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। जजों ने इस वकील को भविष्य में इसका ख्याल रखने की चेतावनी भी दी है। भारत के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को काले कोट के ऊपर एक काला लबादा भी पहनना पड़ता है जो कि एक कॉमिक्स, मैनड्रेक के मुख्य किरदार एक जादूगर के लबादे की तरह रहता है। हिन्दुस्तानी अदालतों में यह सिलसिला उन अंग्रेजों के वक्त से शुरू हुआ था जिन्होंने इस हिन्दुस्तान को गुलाम बनाकर कुचला था, और जो अपने ठंडे देश की जरूरत की मुताबिक कपड़े पहनने के आदी थे, और उन्होंने हिन्दुस्तान में भी जहां-जहां अदालती और सरकारी रीति-रिवाज बनाने थे, उसी किस्म के बनाए थे। वही ड्रेस लागू किया था जो कि उनके सर्द माहौल में जरूरी था। लोगों ने अंग्रेजी अदालतों के जजों की तस्वीरें फिल्मों और टीवी सीरियलों में देखी होंगी कि वे किस तरह कोट के ऊपर लबादा पहनकर और सिर पर ऊन की एक विग लगाकर बैठते हैं ताकि उनका सिर ठंड से बचा रहे। जिस हिन्दुस्तान के अधिकतर हिस्से में गर्मी और बहुत गर्मी नाम के दो मौसम रहते हैं, वहां पर वकीलों पर काले कोट के ऊपर काला लबादा पहनकर ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की बंदिश शर्मनाक है।
हिन्दुस्तान की छोटी अदालतों में भी देखें तो जहां पर भरी गर्मी में भी वकीलों के लिए ठंडक का कोई इंतजाम नहीं रहता, और जहां पर वे एक अदालत से दूसरी अदालत दौड़ते हुए लू के थपेड़ों का सामना करते हैं, वहां भी उनसे काला कोट पहनने को कहा जाता है, और बहुत से गरीब वकील तो ऐसे रहते हैं जिनके काले कोट पर पसीने के सफेद दाग से मानो मुल्क का नक्शा ही बन जाता है। कुछ ऐसा ही हाल भारत की रेलगाडिय़ों में अंग्रेजों के समय से टिकट जांचने वाले अधिकारियों का है जिन्हें काला कोट पहनने की बंदिश रहती है, और बिना एसी वाले डिब्बों से लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म तक भट्टी की तरह तपते रहते हैं। कुछ ऐसा ही हाल हिन्दुस्तान में पुलिस का है जिसे अंग्रेजों के समय से चमड़े के जूते पहनाना शुरू हुआ, तो वह आज भी जारी है, जबकि आज कई किस्म के आरामदेह जूते चलन में आ गए हैं, लेकिन जिस पुलिस से दौड़-भाग और कामकाज की उम्मीद की जाती है, उसे चमड़े के कड़े जूते पहनने को कहा जाता है जिस पर पॉलिश करने का बोझ भी रहता है।
आजादी की पौन सदी पूरी हो रही है, लेकिन हिन्दुस्तान अब तक सिर उठाकर जीना नहीं सीख पाया है। वह अंग्रेजों के छोड़े गए पखाने को अपने सिर पर एक टोकरे की तरह सजाकर खुश है। देश की नौकरशाही को देखें तो वह बंद गले का कोट या सूट और टाई लगाकर लाट साहब बनकर जनता के पैसों की एयरकंडीशनिंग बर्बाद करती है। किसी शासकीय या राजकीय समारोह में अफसरों को बंद गले का कोट पहने देखकर ही तन-बदन में आग लगने लगती है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, या देश के मुख्य न्यायाधीश के आने पर, या किसी और देश के किसी प्रमुख का स्वागत करने के लिए तैनात अफसरों को मई-जून की 45 डिग्री की तपती हुई भट्टी में भी कोट या सूट पहनने की बंदिश बुनियादी मानवाधिकारों के भी खिलाफ है, लेकिन देश की किसी अदालत को यह बात नहीं खटकती, और वे राजसी-सामंती महत्व पाना चाहती हैं। ऐसे जितने लोग दिखावे के इस आडंबर के लबादे ढोते हैं, उनकी वजह से उनके घर, दफ्तर, समारोह की जगहों पर अंधाधुंध एसी चलाकर उन्हें ठंडा रखा जाता है ताकि वे कोट-जॉकिट, और लबादों के भीतर भी गर्मी महसूस न करें। कुल मिलाकर अंग्रेजों की इस उतरन को आज भी हिन्दुस्तानी राजकीय, शासकीय, और अदालती परंपरा बनाने की कीमत आम जनता चुकाती है, जो कि इन जगहों के बिजली के बिल देती है। अदालतों के जानकार कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट वहां के साल के कुछ सबसे गर्म महीनों में वकीलों को लबादे से छूट देती है। लेकिन कई हाईकोर्ट अंग्रेजों की छोड़ी परंपराओं के इतने बड़े भक्त हैं कि वहां किसी नए मुख्य न्यायाधीश को शपथ लेते समय ऊनी विग भी पहननी पड़ती है जो कि अंग्रेजों के अपने देश में तो बर्फीले मौसम में जजों के सिर के लिए हिफाजत की चीज थी, लेकिन हिन्दुस्तान जैसे गर्म देश में जो एक गंदे बोझ के अलावा कुछ नहीं है।
एक आजाद देश में यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। आम जनता जो कि पिछले कई जन्मों के बुरे कामों की वजह से आज अदालत में फंसती है, वह वैसे भी अदालती माहौल देखकर दहशत में रहती है। उसके बाद जब लबादा पहने हुए वकील उससे बात करते हैं, तो वह अपने या सामने वाले वकील को जादूगर की तरह मानने को मजबूर हो जाती है। ये सारे सामंती प्रतीक हिन्दुस्तान की अदालतों से, राष्ट्रपति भवन और राजभवनों से खत्म किए जाने चाहिए। यह देश गरीबों का देश है, और यहां पर साधनों की ऐसी बर्बादी भी ठीक नहीं है, और न ही वकीलों, खुद जजों, और दूसरे सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों पर पोशाक की ऐसी बंदिश लागू करनी चाहिए जो कि यहां के मौसम के खिलाफ है। देश के कई विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोहों में ऐसे ही लबादों का चलन खत्म कर दिया गया है, और उनकी जगह हिन्दुस्तानी संस्कृति की पोशाक लागू की गई है, जो कि एक बेहतर समझदारी का फैसला है। देश के बाकी तबकों को भी इससे सबक लेना चाहिए, और अंग्रेजों की गंदगी को ढोना अगर बंद किया जाए तो देश की बहुत सी बिजली भी बच सकती है।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
यूक्रेन पर रूस के हमले पर दुनिया बंटी हुई है। हिन्दुस्तान और चीन जैसे कई देश अपनी-अपनी अलग-अलग वजहों से इस मामले पर शांत हैं, पश्चिमी देश और योरप रूस के खिलाफ है, और बाकी देशों का भी अलग-अलग रूख है। खुद अमरीका के भीतर यूक्रेन को लेकर अमरीकी नीति बंटी हुई है, और कुछ प्रमुख लोगों का यह मानना है कि अमरीकी सरकार वहां जो कर रही है वह नाकाफी है। लेकिन रूस के मुहाने पर बैठे हुए योरप के नाटो देश अधिक खतरा उठाने की हालत में नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अगर यह युद्ध बढ़ेगा, और रूस अगर दूसरे देशों पर भी जवाबी हमला करेगा तो वह द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद का सबसे बड़ा युद्ध हो जाएगा, और वह तीसरा विश्वयुद्ध भी हो सकता है। ऐसे में सारे देश चौकन्ना होकर काम कर रहे हैं, यूक्रेन को नागरिक मदद कर रहे हैं, कुछ फौजी मदद भी भेज रहे हैं, लेकिन न तो अमरीका और न ही नाटो देश अपनी फौज वहां भेज रहे हैं। दरअसल किसी भी देश की फौज वहां पहुंचने का मतलब रूस को इस बात का हक देना हो जाएगा कि वह उन देशों पर भी हमला कर सके। तनाव को इतना बढऩे देने से सारे लोग कतरा रहे हैं।
लेकिन आज नाटो और अमरीका की तरफ से जो फौजी हथियार यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, उनके खतरे को समझना होगा। आज बाहर से कोई फौजी मदद मिले बिना यूक्रेन रूस के सामने जल्दी कमजोर पड़ता, और वह या तो हार जाता, या कोई संधि विराम होता। इन दोनों ही स्थितियों में यूक्रेन की जनता मरने से बचती, और यूक्रेनी शहरों की जो भयानक तबाही अभी चल रही है, वह भी थमती। यूक्रेन अपनी ताकत से लडऩे लायक रहता तो लड़ता या फिर रूस के सामने समर्पण कर देता। दोनों तरफ की मौतें थमतीं, और यूक्रेन के ढांचे की तबाही भी थमती। लेकिन अमरीका और योरप जिस तरह का फौजी साज-सामान यूक्रेन को भेज रहे हैं उसका एक मकसद यह भी दिखता है कि वे यूक्रेन को इस मोर्चे पर डटाए रखना चाहते हैं ताकि उसके हाथों रूस की जितनी तबाही हो सके, उतनी हो जाए। पश्चिम के देश रूस पर लगाए आर्थिक प्रतिबंधों के असर का भी इंतजार कर रहे हैं, जिसमें महीनों लग सकते हैं। लेकिन इस बीच वे रूस को कमजोर भी करना चाहते हैं, इसलिए वे बिना अपनी फौजों को भेजे सिर्फ यूक्रेन को मोर्चे पर डटाए चल रहे हैं। रूस का नुकसान करने की नीयत पूरी करने के लिए नाटो और अमरीका यूक्रेन के जनता और इस देश को कोलैटरल डैमेज बना रहे हैं। नाटो और अमरीका के पास इस बात का पूरा अंदाज है कि इस मोर्चे के जारी रहने से रोज दोनों तरफ कितनी मौतें हो सकती हैं, यूक्रेन का कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन रूसी फौजों का नुकसान, और रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए नाटो और अमरीका इस जंग को चलने देना चाहते हैं।
यह बात कुछ लोगों को विरोधाभासी लग सकती है क्योंकि यूक्रेन से निकल रहे, और निकलने वाले दसियों लाख शरणार्थियों का बोझ योरप के देशों पर ही पडऩे वाला है, लेकिन वह एक नागरिक बोझ रहेगा, और रूस को फौजी और आर्थिक रूप से कमजोर करने की रणनीति एक अलग बात है। आज अगर नाटो-अमरीका की हथियारों की यह मदद नहीं रहती, तो शायद यूक्रेन की जंग कुछ जल्द खत्म हो गई रहती। किसी की मदद करने का यह अनोखा तरीका है जिसमें उसके अधिक दूर तक नुकसान पाने की गारंटी हो रही है। आज चारों तरफ इस मुद्दे पर अपनी कोई राय बनाने के पहले हर सरकार यह सोच रही है कि इस जंग से उसे क्या नफा या नुकसान हो रहा है। अब जैसे पंजाब की नई सरकार को लेकर एक नई अटकल सामने आई है कि दुनिया में गेहूं का दाम दो से चार गुना तक बढ़ चुका है क्योंकि रूस और यूक्रेन गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक थे, और ऐसे हाल में पंजाब की नई सरकार को चाहिए कि वह दुनिया में गेहूं निर्यात करके एक मोटा मुनाफा कमाने की कोशिश करे ताकि उसके किसानों को फायदा हो सके। ऐसा हाल पेट्रोलियम, गैस, खाने का तेल, कई तरह के खनिज, बहुत किस्म की धातुओं को लेकर भी है कि रूस और यूक्रेन से निर्यात ठप्प होने पर किस-किस देश की क्या नई संभावना बनेगी? सोचा तो यहां तक जा रहा है कि रूस से पेट्रोलियम बहिष्कार जारी रखने के लिए क्या दुनिया ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को ढीला करे, और क्या ईरानी पेट्रोलियम से दुनिया की कमी को पूरा किया जा सके? दो देशों के बीच जंग में उनका सीधा नुकसान जो भी हो रहा हो, बाकी दुनिया को कई किस्म का नुकसान भी हो रहा है, और उसकी भरपाई के लिए भी उन्हें कई किस्म के फायदे कमाने के रास्ते निकालने का हक है।
लोगों को यह भी लग रहा है कि रूस अगर एक वक्त के सोवियत संघ का अपना हिस्सा रहा हुआ यूक्रेन फिर से कब्जा कर पाता है, तो क्या उससे ताईवान पर कब्जा करने की चीन की बहुत पुरानी, और हमेशा जिंदा हसरत को एक नई ताकत मिलेगी? क्या इससे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के कुछ विवादित हिस्सों को लेकर एक नए तनाव की हसरत खड़ी हो सकेगी? और आज लोगों को यह भी लग रहा है कि इस तनाव के बीच रूस और चीन के बीच संबंध जितने बेहतर हो रहे हैं, क्या वह अमरीका और उसके साथी देशों के लिए एक नया खतरा बन सकता है? ऐसे सौ किस्म के सवाल सौ देशों के सामने है, और वे अपने-अपने हितों को देखते हुए यह सोचते हैं कि रूस की हार या रूस की जीत में से उनका फायदा किसमें है? और रूस का अगर नुकसान करना उनके फायदे में है तो वह अपने लोगों की जिंदगी दांव पर लगाए बिना कैसे किया जा सकता है? आज की एक चर्चा यह भी है कि रूस में सत्ता के कुछ खरबपति कारोबारी लोगों की भाड़े के सैनिकों की निजी फौज को भी यूक्रेन भेजा गया है ताकि वे राष्ट्रपति और उनके परिवार को मार सकें। रूसी सरकार ऐसी किसी निजी फौज के अस्तित्व से हमेशा इंकार करती रही है, लेकिन सीरिया की जंग से लेकर कांगो के फौजी मोर्चे तक ये भाड़े के रूसी सैनिक कारोबारियों द्वारा भेजे जाते रहे हैं, और वे रूसी सरकार की रणनीति में साथ देने का काम करते रहे हैं। इसलिए ऐसी बहुत सारी जानकारी यह बताती है कि रूस और यूक्रेन की यह जंग, या रूस का यूक्रेन पर यह हमला बाकी दुनिया के लिए शतरंज की बिसात पर चाल चलने जैसा हो गया है, और इस मुद्दे का अतिसरलीकरण करना ठीक नहीं है।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
छत्तीसगढ़ के बस्तर में बेकसूर और निहत्थे आदिवासियों की सुरक्षा बलों के हाथों मौत एक आम बात है। हर बरस कई ऐसे कत्ल होते हैं लेकिन चूंकि कातिल सरकारी वर्दीधारी रहते हैं, और वे लोकतंत्र को बचाने के नाम पर लोगों का कत्ल करते हैं इसलिए उस कत्ल को हत्या न कहकर नक्सल-संदेह में हुई मौत कह दिया जाता है, या कभी यह कह दिया जाता है कि सुरक्षा बलों ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं जिनमें ये मौतें हो गईं, या नक्सलियों के साथ क्रॉस फायरिंग में ये ग्रामीण मारे गए। सबसे अधिक तो यही होता है कि पुलिस और सुरक्षा बल इस बात पर अड़े रहते हैं कि मारे गए लोग नक्सली थे, उनके पास कुछ हथियार भी रखकर जब्ती दिखा दी जाती है। लेकिन बहुत से मामले ऐसे रहते हैं जिनमें शक की गुंजाइश नहीं रहती है, जिनमें सरकार भी भारी जन-दबाव में किसी जांच के लिए मजबूर होती है। जब-जब ऐसी जांच होती है तब-तब यह सामने आता है कि सुरक्षा बलों ने बिना किसी खतरे के, बिना किसी उकसावे और भडक़ावे के निहत्थे और बेकसूर ग्रामीण आदिवासियों को मार डाला था।
ऐसी ही एक वारदात 2013 में बीजापुर जिले के जगरगुंडा थाना-इलाके के एडसमेटा गांव में हुई थी जिसमें 8 बेकसूर आदिवासियों को सुरक्षा बलों ने मार डाला था, जिनमें तीन बच्चे भी थे। इस मामले की न्यायिक जांच एमपी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज, जस्टिस वी.के. अग्रवाल ने की थी, और कल यह रिपोर्ट छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश की गई है। इस रिपोर्ट का नतीजा यह है कि समारोह मनाते आदिवासियों की जिस भीड़ पर सीआरपीएफ ने गोलियां चलाई थीं, उन सुरक्षा-जवानों को इन आदिवासियों से कोई खतरा नहीं था। न इन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई थीं, न हमला किया था। इसलिए सीआरपीएफ ने ये गोलियां आत्मरक्षा में नहीं चलाईं बल्कि आदिवासियों को पहचानने में हुई गलती और घबराहट के कारण चलाईं।
जैसा कि आमतौर पर इस किस्म के जांच आयोग आदिवासी जिंदगी से नावाकिफ शहरी जजों वाले होते हैं, इसलिए इनमें आदिवासी जिंदगियों के लिए वह दर्द नहीं होता जो कि आदिवासियों के जानकार किसी हमदर्द का हो सकता है। थोक में किए गए ऐसे कत्ल भी सजा नहीं पाते हैं क्योंकि सरकारें इस बात से डरती हैं कि बेकसूरों के कत्ल के जुर्म में अगर सुरक्षा बलों को सजा होने लगे, तो ऐसे हथियारबंद मोर्चों पर उनका मनोबल टूटेगा। यह सोच निहायत ही अलोकतांत्रिक और शहरी सोच है जिसमें निहत्थे और बेकसूर आदिवासियों के कत्ल की कीमत पर भी वर्दी का मनोबल बनाए रखने को जरूरी समझा जाता है। और बस्तर के मामले में हमने बार-बार ऐसी सोच देखी है, कोई भी पार्टी सरकार चलाए, सत्ता की सोच तकरीबन एक सरीखी दिखती है। सत्तारूढ़ पार्टी और सुरक्षा बलों के हित मानो एक हो जाते हैं, और नक्सल-संदेह में कितने ही बेकसूर आदिवासियों का कत्ल माफ कर दिया जाता है। जांच के नाम पर, जांच आयोग के नाम पर ऐसी लीपापोती की जाती है कि किसी कातिल को कोई सजा मिल ही नहीं पाती। अब 2013 के इस हत्याकांड की जांच रिपोर्ट का कवर पेज ही कहता है- एडसमेटा में मुठभेड़ की घटना के मामले में न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन। जबकि यह रिपोर्ट खुद ही लिख रही है कि यह साबित नहीं हुआ है कि उक्त मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई, और आगे यह साफ होता है कि घटना सुरक्षा बलों द्वारा आग के आसपास इक_े लोगों को देखकर उन्हें संभवत: गलती से नक्सल समझकर घबराहट की प्रतिक्रिया के कारण गोलियां चलाने के कारण हुई।
अब सवाल यह उठता है कि वर्दीधारी सुरक्षा बलों का पूरा जत्था पूरी तैयारी से जंगल गया हुआ है, और वहां पर निहत्थे आदिवासियों को देखकर वह इतना हड़बड़ा रहा है कि वह उन पर गोलियां चलाकर 8 लोगों को मार डाल रहा है जिनमें नाबालिग भी थे। तो यह सुरक्षा बलों की कैसी तैयारी है, और यह कैसी घबराहट है जिसके चलते बेकसूरों को भून दिया गया? यह पूरा सिलसिला बताता है कि आदिवासी जिंदगी इतनी सस्ती है कि नक्सलियों को मारने के नाम पर जंगल में बसे हुए मासूम और सीधे-साधे, निहत्थे आदिवासियों को भी महज अपने संदेह के आधार पर मार डाला जा सकता है। अगर सुरक्षा बल किसी के नक्सली होने की आशंका में इतने घबरा सकते हैं कि वे उन्हें गोलियों से भून सकते हैं, तो फिर ऐसी हालत में सरकार को यह नीतिगत फैसला लेना चाहिए कि ऐसे डरे-सहमे सुरक्षा बल को ग्रामीण इलाकों में भेजा ही क्यों जाए? खुद जांच रिपोर्ट की भाषा और उसके निष्कर्ष न छुपने लायक तथ्यों को तो मानो मजबूरी में सामने रख रहे हैं, लेकिन किंतु-परंतु जैसे शब्दों के साथ संदेह का इतना लाभ सुरक्षा बलों को दे रहे हैं कि मानो वह किसी चुनाव के पहले किसी सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा दिया गया चुनावी तोहफा हो। सुरक्षा बलों द्वारा घबराहट में गोली चलाना इस रिपोर्ट में इतनी बार इतने तरह से लिखा गया है कि ऐसा लगता है कि बेकसूर आदिवासियों की लाशों से भी अधिक ठोस सुबूत इस घबराहट का है। बार-बार इस घबराहट का हवाला देना एक किस्म से कातिल सिपाहियों को बचने के लिए एक रास्ता देना है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के आधार पर इसकी जांच 2019 में सीबीआई को दे दी गई थी, और वह जांच चल रही है। उस जांच, और उसके नतीजे के बारे में अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन यह अकेला मामला नहीं है जिसने बस्तर में बेकसूर आदिवासियों को थोक में मारा है। इससे पहले भी राज्य की पुलिस द्वारा आदिवासी गांवों को जलाने और लोगों को मारने के मामले सामने आ चुके हैं, महिलाओं से बलात्कार के मामले भी सामने आ चुके हैं, और विपक्ष में रहते हुए जो कांग्रेस आदिवासियों की हमदर्द थी, वह सत्ता में आने के बाद अपने कार्यकाल के ऐसे जुर्म जायज ठहराने में लगी दिखती है। यह मौका जनसंगठनों द्वारा नक्सल कहलाने का खतरा उठाते हुए भी ऐसी सरकारी हिंसा को उजागर करने का है जिसके बिना आदिवासियों के बचने की और कोई गुंजाइश नहीं है। बस्तर को लेकर यह सरकारी फैशन है कि आदिवासियों की हमदर्द कोई भी बात, उनका कोई भी आंदोलन, नक्सलियों का करवाया हुआ मान लिया जाता है। सत्ता का चरित्र एक ही होता है, प्रदेश में भाजपा की सरकार गई, और कांग्रेस की सरकार आई, ये दोनों ही सरकारी सुरक्षा बलों की हिमायती रहीं, और बेकसूर आदिवासियों के कत्ल पर इनकी हमदर्दी की कमी एक बराबर रही। इसलिए जांच आयोग के इस प्रतिवेदन से सरकारी सुरक्षा बलों के चाल-चलन पर कोई फर्क पड़ेगा, ऐसी उम्मीद गलत होगी। सीबीआई जांच के बाद कुछ लोगों को सजा मिल सके, तो उसमें अभी से कई बरस लगना बाकी है। आदिवासियों की मौत इसी तरह जारी रहेगी, और शहरी लोकतंत्र के पास उनके लिए गोलियां ही हैं।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत और जनता द्वारा कांग्रेस सरकार की बुरी तरह बर्खास्तगी लोगों को हैरान कर गई है। इसके साथ-साथ जिस तरह वहां अकाली दल और भाजपा किनारे कर दिए गए हैं, इन तीनों पार्टियों के सारे के सारे बड़े नेता जनता ने हरा दिए हैं, वह भी चौंकाने वाली नौबत है। बहुत से लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार आते दिख रही थी, लेकिन वह ऐसे अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बहुमत के साथ आएगी इसका अंदाज कई लोगों को नहीं था, या बेहतर यह कहना होगा कि शायद किसी को नहीं था। वहां पर लोग पांच कोने का संघर्ष देख रहे थे जिनमें ऊपर लिखी गई चारों पार्टियों के अलावा किसान उम्मीदवार भी एक ताकत माने जा रहे थे, लेकिन जनता ने खुलकर दो बातें साफ कीं, एक तो यह कि उसने कांग्रेस, भाजपा और अकाली, पंजाब में सत्तारूढ़ रही इन तमाम पार्टियों को पूरी तरह खारिज कर दिया, और आम आदमी पार्टी के नारे के मुताबिक एक मौका केजरीवाल को दिया है।
अब आप की सरकार पंजाब में चुनौतियों के एक टोकरे के साथ काम शुरू कर रही है। पंजाब की अर्थव्यवस्था खराब हालत में है, बेरोजगारी आसमान छू रही है, नौजवानों में नशा पंजाब के हर दूसरे-चौथे घर को बर्बाद कर चुका है, उद्योग लग नहीं रहे हैं, और किसान कानून वापिस होने के बावजूद पंजाब में किसानों की यह हकीकत तो दर्ज है ही कि वहां देश में सबसे अधिक किसान आत्महत्याएं हो रही हैं। इसके साथ-साथ पंजाब के बारे में यह बात भी कही जाती है कि वहां के लोग अपनी सरकार पर दिल्ली से राज पसंद नहीं करते। ऐसे में दिल्ली से चल रही आम आदमी पार्टी का जीता हुआ पंजाब राज्य से कितना चलेगा और दिल्ली से कितना, इसे लेकर भी लोगों में कुछ हैरानी बनी हुई है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि दिल्ली में स्कूल और अस्पताल नाम की जिन दो सहूलियतों को लेकर आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपाती है, वे दोनों चीजें तो कायदे से म्युनिसिपल के करने की रहती हैं, और राज्य सरकार पंजाब में इन बातों को अपनी पूरी कामयाबी नहीं बता पाएगी, दिल्ली में बात कुछ और थी।
दिल्ली को कुछ समझे बिना आम आदमी पार्टी के कामकाज को समझना मुमकिन नहीं है। दिल्ली की सरकार को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं है। उसके पास न पुलिस है, और न जमीनों का हक। दिल्ली के सारे बड़े प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के अधीन आते हैं, और दिल्ली की अधिकतर दूसरी दिक्कतों और संभावनाओं के लिए राज्य सरकार न जिम्मेदार है, न अधिकारसंपन्न। इसके अलावा दिल्ली में स्थानीय म्युनिसिपल और दिल्ली विकास प्राधिकरण, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण जैसे दूसरे संगठन भी हैं जो कि राज्य सरकार से परे काम करते हैं, और वहां राज्य सरकार की संभावनाएं, उसकी स्वायत्तता, सब लेफ्टिनेंट गवर्नर के मातहत रहती हैं, और केजरीवाल सरकार किसी आईएएस का तबादला भी करने का हक नहीं रखती है। बात-बात में उसे एलजी की इजाजत लेनी पड़ती है। इसलिए केजरीवाल सरकार दिल्ली को एक बड़े म्युनिसिपल की तरह चला रही थी, और केजरीवाल एक म्युनिसिपल कमिश्नर अफसर की तरह काम कर रहे थे। पंजाब एक अलग मामला है, और दिल्ली का प्रयोग पंजाब में बहुत ही सीमित उपयोग का है।
पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री बन रहे भगवंत मान का सरकार चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है, और उन्हें विरासत में एक भयानक भ्रष्ट और घाघ नौकरशाही मिल रही है, जिससे काम लेना एक बड़ी चुनौती रहेगी। केजरीवाल के साथ म्युनिसिपल जैसी दिल्ली चलाते भी यह सहूलियत थी कि वे आईआईटी से पढक़र निकले हुए इंजीनियर थे, और भारत सरकार में एक बड़ी नौकरी करते हुए पहले सामाजिक आंदोलन, और फिर राजनीति में आए थे। उनकी पत्नी भी इसी बड़ी सरकारी नौकरी में थीं। यानी उनके पास सरकार के कामकाज का कुछ तजुर्बा था, और वह सहूलियत भगवंत मान को हासिल नहीं है। दिल्ली और पंजाब की कई दिक्कतों पर एक-दूसरे से टकराव की नौबत भी है। पंजाब में किसानों को फसल के ठूंठ, पराली, जलाने की मजबूरी है, और दिल्ली लगातार इसका विरोध करते आई है कि इससे दिल्ली की हवा दमघोंटू और जहरीली हो जाती है। अब दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार रहने से इसका क्या होगा, यह भी सोचने की बात है। पंजाब की शक्ल में आम आदमी पार्टी को अपने इतिहास में पहली बार एक पूर्ण राज्य चलाने का मौका मिल रहा है, और उसकी दिल्ली की कामयाबी का पैमाना इस राज्य में काम नहीं आने वाला है। पंजाब की चुनौतियां भी अलग हैं, और संभावनाएं भी। हो सकता है कि आप सरकार पंजाब में दिल्ली से अधिक कामयाब भी हो जाए, या बहुत हद तक फ्लॉप भी हो जाए। पंजाब में सरहद पाकिस्तान से लगी हुई है, और वहां से नशे की तस्करी के अलावा आतंक का खतरा भी लगातार बने रहता है। पहली बार पुलिस सम्हालने जा रही आम आदमी पार्टी के सामने यह सरहद भी चुनौती रहेगी क्योंकि इसके किनारे की बहुत चौड़ी पट्टी राज्य की पुलिस के अधिकार क्षेत्र से परे बीएसएफ के हाथ रहती है, और यह राज्य और केन्द्र के बीच टकराव का एक मुद्दा रह सकती है, ठीक उसी तरह जिस तरह कि केजरीवाल सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट तक जाकर दिल्ली सरकार से टकराव के कई प्रयोग किए थे, और उन सबमें उसकी हार हुई थी। दिल्ली में चुनौतियां भी सीमित थीं, और संभावनाएं भी, पंजाब में ये दोनों असीमित हैं, और विरासत में एक बदहाल राज्य मिला है।
पंजाब को आम आदमी पार्टी की दिल्ली की पहली जीत के बाद का सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे इस पार्टी की देश भर की संभावनाएं भी खुलती हैं, और वह कांग्रेस और भाजपा के एक विकल्प के रूप में भी कहीं-कहीं कोशिश कर सकती है, यह एक और बात है कि बहुत से राजनीतिक विश्लेषक भी इस पार्टी को संघ परिवार का एक मुखौटाधारी संगठन मानते हैं, और यह मानते हैं कि आखिर में जाकर यह किसी चुनौती की नौबत रहने पर भाजपा के ही हाथ मजबूत करने का काम करेगी। भाजपा को आप की पंजाब जीत इस हिसाब से भी बुरी नहीं लग रही होगी कि उसने कांग्रेस की सरकार को बेदखल किया है, और भाजपा से अलग हुए अकालियों को भी मटियामेट कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के साथ आम आदमी पार्टी का किस तरह का तालमेल रहेगा, इस पर भी लोगों की निगाह रहेगी, हो सकता है कि यह तालमेल तुरंत शुरू न हो, और भाजपा के किसी नाजुक मौके के लिए बचाकर रखा जाए। फिलहाल आम आदमी पार्टी के सामने पंजाब दिल्ली के मुकाबले कई गुना अधिक बड़ी चुनौती है, और उसे केजरीवाल जैसा सरकारी कामकाज का जानकार भी हासिल नहीं है। आगे-आगे देखें होता है क्या?
यूपीए सरकार के वक्त भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे और मशहूर अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण महंगाई बढ़ेगी, और यह लंबे समय तक रहेगी, इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कई चीजों के दामों में इस युद्ध से बढ़ोत्तरी हो चुकी है, और कई देशों में पहले से ही महंगाई अधिक थी, अब इन दोनों के मिले-जुले असर को देखें तो यह महंगाई और मंदी लंबी चलेंगी। उन्होंने कहा कि रूस ऊर्जा सहित दूसरे कई सामानों का एक बड़ा एक्सपोटर है और रूस पर पश्चिमी देशों के लगाए हुए आर्थिक और कारोबारी प्रतिबंध से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
आज दुनिया में दिक्कत यह है कि अर्थव्यवस्था के पैमाने आम इंसानों की जिंदगी से काटकर अलग कर दिए गए हैं। जब किसी देश में बेरोजगार आसमान पर पहुंच रही है, महंगाई चरम पर है, लोग सरकारी रियायती अनाज के बिना भुखमरी की हालत में हैं, तब अगर उस देश का शेयर बाजार आसमान पर पहुंचता है, तो क्या उसे सचमुच ही देश की अच्छी और मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत मान लिया जाए? हिन्दुस्तान इसकी एक बड़ी मिसाल है कि यहां पर जनता जब से बदहाल है, तब शेयर बाजार सबसे खुशहाल है। इसलिए अर्थव्यवस्था के पैमानों को अलग-अलग देखने की जरूरत है कि शेयर बाजार का रूझान और जनता की हकीकत के बीच क्या फर्क है? ऐसा न होने पर अंबानी-अडानी की कमाई को आम जनता की कमाई से जोडक़र औसत निकालकर आम जनता को खुशहाल साबित किया जा सकता है। इसलिए आज अगर हिन्दुस्तान में 20 लाख की कार के लिए 50 हजार लोग कतार में लगे हैं, तो इसे आम जनता की खुशहाली मान लेने की गलती नहीं करनी चाहिए।
रघुराम राजन की बातों से परे भी यह समझने की जरूरत है कि दुनिया की एक बड़ी जंग हो, या कि मौसम की सबसे बुरी मार हो, सबसे अधिक जख्म सबसे कमजोर तबकों को आते हैं। बाढ़ हो या तूफान, उसमें सबसे अधिक तबाही सबसे गरीब आबादी की होती है क्योंकि वे ही लोग सबसे नाजुक और खतरनाक जगहों पर बसे होते हैं। जब सूखा पड़ता है और उसकी वजह से लोगों को अपना इलाका छोडक़र, घर-बार छोडक़र बाहर जाना पड़ता है, तो सूखे की सबसे बुरी मार सुखी तबके पर नहीं पड़ती, गरीबी से दुखी तबके पर पड़ती है जो कि एक मौसम का सूखा झेलने की हालत में भी नहीं रहता। आज अगर हिन्दुस्तान में आधी आबादी रियायती सरकारी अनाज की वजह से जिंदा है, तो यह जिंदा रहना भी क्या जिंदगी है? जिस संसद को इस गरीबी पर सोच-विचार करना था, लोगों को इससे उबारने की कोशिश करनी थी, वह संसद अपने आप पर 20 हजार करोड़ रूपए खर्च करने जा रही है, इसके मुखिया मुल्क के प्रधानमंत्री अपने लिए 8 हजार करोड़ रूपए का विमान खरीद रहे हैं। ऐसे में अदम गोंडवी की लिखी एक गजल याद पड़ती है-
सौ में सत्तर आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं,
दिल पे रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है?
दुनिया या किसी देश की अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय आंकड़ों से आंकने का सिलसिला ही नाजायज है। गरीबों की आर्थिक स्थिति को अलग से आंकने के पैमाने बिल्कुल साफ रहने चाहिए, और दुनिया या किसी भी देश में गरीब आधी आबादी के हाल पर अलग से रिपोर्ट बननी चाहिए। हिन्दुस्तान में आज जीडीपी या सकल राष्ट्रीय उत्पादन की शक्ल में देश के हाल को आंका जाता है, लेकिन अडानी और अंबानी की दौलत दो या तीन गुना हो जाने से देश की नीचे की आधी आबादी की जिंदगी पर कोई फर्क पड़ सकता है क्या? क्या बाजार में एक करोड़ रूपए से अधिक दाम वाली कारों की बिक्री दोगुना हो जाने से मोपेड चलाने वाले गरीब की पेट्रोल खरीदने की ताकत को भी दोगुना आंकना ठीक होगा? यह पूरा सिलसिला आंकड़ों का फरेब है, और अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को लेकर जनसंगठनों को यह मांग करनी चाहिए कि गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों की अर्थव्यवस्था, उनकी आर्थिक हालत पर अलग से रिपोर्ट जारी की जानी चाहिए जिस तरह कि एक वक्त अलग से रेल बजट आता था। आज केन्द्र और प्रदेश सरकार को आर्थिक विकास के तमाम आंकड़ों में से बीपीएल समुदाय के आंकड़े अलग से सामने रखने चाहिए, लोगों को बीपीएल से जुड़े आंकड़े अलग से पूछने चाहिए। जब तक गरीबों के हिमायती पैमाने अलग से लागू नहीं होंगे, तब तक हिन्दुस्तान जैसे देश में दो सबसे अमीर लोगों की तिजोरियों को गरीबी की रेखा के नीचे की हंडियों को भरा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहेगा।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
भारत और पाकिस्तान के बीच दो दिन पहले अपने किस्म की एक अनोखी और पहली वारदात हुई, भारत की एक मिसाइल गलती से चली और पाकिस्तान में जाकर गिरी। यह चालीस हजार फीट की ऊंचाई तक गई और पाकिस्तानी सरहद के भीतर सवा सौ किलोमीटर तक जाकर गिरी। गनीमत यही कि इतने लंबे हवाई सफर में इस मिसाइल ने न तो किसी हवाई जहाज को निशाना बनाया, और न ही कोई इंसान इसकी चपेट में आए। जैसा कि जाहिर है, पाकिस्तान ने इस पर जमकर नाराजगी जाहिर की है, और भारत ने इस बारे में इतना ही कहा है कि नौ मार्च को मिसाइल के नियमित रखरखाव के दौरान तकनीकी खामी के चलते मिसाइल अचानक फायर हो गई, इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, यह पता लगा है कि पाकिस्तान में जाकर गिरी है, यह दुखद घटना है, लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें कोई मौत नहीं हुई।
यह मामला बड़ा अटपटा है। इसके पहले कम से कम से हिन्दुस्तान और उसके पड़ोसियों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यह भी अच्छी बात है कि सात मिनट में आसमान में उडऩे वाली इस सुपर सोनिक मिसाइल ने किसी भी विमान को चपेट में नहीं लिया, और न ही आबादी पर, या किसी नाजुक ठिकाने पर गिरी। तकनीकी चूक किसी भी जगह हो सकती है, लेकिन यह तकनीकी चूक अगल-बगल के, दुश्मन सरीखे रह गए दो परमाणु देशों के बीच हुई है जो कि एक बड़ा तनाव खड़ा कर सकती थी। अब किसी तकनीकी चूक पर तो अधिक लिखना ठीक नहीं है लेकिन यह समझने की जरूरत है कि अड़ोस-पड़ोस के दो देशों के बीच अगर गैरजरूरी तनाव फैले रहें तो उसमें ऐसी कोई घटना बहुत बड़ा टकराव शुरू कर सकती थी, और ऐसे ही मौकों को टालने के लिए लोगों के बीच रिश्ते बेहतर रहने चाहिए। यह मानकर चलना चाहिए कि तकनीकी या मानवीय चूक कभी भी, और कहीं भी हो सकती है, इसलिए तनाव को कम रखना ही अकेला जरिया है जिससे दुश्मनी पाल रहे दो देशों के बीच टकराव टल सके।
भारत और पाकिस्तान ने समय-समय पर कुछ बर्दाश्त भी दिखाया है, और अपनी-अपनी घरेलू राजनीति में लुभावने उकसावे के बावजूद इन देशों ने कभी एक-दूसरे के गलती से आ गए लोगों को भी तोहफे देकर सरहद पार भेजा है, और दोनों देशों की सरकारों के बीच हाल के कई महीनों में कोई नया टकराव नहीं हुआ है। इसलिए आज गलती से चली इस मिसाइल के बहाने से हम यह चर्चा करना चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान को एक-दूसरे से बातचीत का सिलसिला फिर शुरू करना चाहिए। एक-दूसरे से टकराव और सरहद पर गोलाबारी राजधानी में बैठे फौजी अफसरों और नेताओं को तो माकूल बैठ सकती है, हथियार कंपनियों और जंग के सौदागरों को भी वह सुहा सकती है, लेकिन दोनों देशों की जनता सरहद के तनाव का बड़ा दाम चुकाती हैं। दोनों देशों में गरीबी भरपूर है, यह एक अलग बात है कि पाकिस्तान का हाल अधिक खराब है। लेकिन हिन्दुस्तान में भी गरीबी की रेखा के नीचे आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, और मनरेगा जैसी सरकारी रोजगार योजना की वजह से, मुफ्त सरकारी राशन की वजह से लोग मरने से बच रहे हैं। ऐसे में अगर पड़ोस के देशों से तनाव कम होता है, तो बड़ी-बड़ी फौजी खरीदी भी कम हो सकती है। दुनिया में कई दूसरे ऐसे इलाके हैं जहां पर अड़ोस-पड़ोस के देशों के बीच ऐसे गठबंधन या संबंध हैं कि वे एक-दूसरे से अपने को बचाने के लिए फौजी तैयारी करने को मजबूर नहीं रहते हैं। दुनिया के अलग-अलग इलाकों को बहुत आसान और सरल तुलना एक-दूसरे से नहीं हो सकती है, फिर भी गरीबी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए फौजी फिजूलखर्ची को जहां-जहां घटाया जा सकता है, वह किया जाना चाहिए। भारत का तकरीबन तमाम फौजी खर्च पाकिस्तान और चीन से किसी जंग के खतरे को देखते हुए किया जाता है, यह एक अलग बात है कि पाकिस्तान और चीन, इन दोनों के अलग-अलग फौजी खर्च अड़ोस-पड़ोस के देशों में सिर्फ हिंदुस्तान को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। इस सिलसिले को अगर घटाया जा सके, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का फायदा हो सकता है, इससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती है, गरीबी से जूझा जा सकता है। परंपरागत रूप से इन दोनों देशों के आम और गैरसरकारी लोगों के बीच रिश्ते अच्छे रहते आए हैं, और उस तरफ वापिसी जरूरी है। एक मिसाइल गलती से चलकर, सरहद पार जाकर और गिरकर एक जंग भी छिड़वा सकती थी, और वह एक बातचीत भी शुरू करवा सकती है। इस हिंदुस्तानी मिसाइल के जवाब में पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया सीमित और संतुलित रही। दोनों देशों को तनाव घटाते हुए बातचीत शुरू करने का काम करना चाहिए।
पांच राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाने के बाद आज हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ है कि अब कांग्रेस पार्टी का क्या होगा। जो लोग कांग्रेस पार्टी के शुभचिंतक हैं वे भी यह सोचने में लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? इन दोनों का सवालों का जवाब आसान नहीं है। लोगों को याद रखना चाहिए कि कुछ दशक पहले भाजपा लोकसभा में कुल दो सीटों वाली थी, देश के आधी राजनीतिक दलों को उससे परहेज था, लेकिन वहां से चलकर उसने इतना लंबा सफर तय किया है। इसलिए आज कुछ दर्जन लोकसभा सीटों वाली कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य हो ही नहीं सकता यह मान लेना जायज नहीं होगा, लेकिन यह सोचना जरूरी होगा कि इसका कोई भविष्य हो कैसे सकता है?
कांग्रेस पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव को हारने के बाद से करीब दो बरस बिना अध्यक्ष के गुजार चुकी है। राहुल गांधी न केवल खुद इस ओहदे से अलग हुए, बल्कि उन्होंने खुलकर यह कहा कि सोनिया परिवार से परे लीडरशिप देखी जाए। लेकिन बिना इस परिवार की लीडरशिप के हीनभावना से कांपने वाली इस पार्टी ने घूम-फिरकर सोनिया गांधी को ही कामचलाऊ जिम्मेदारी दी, और अब माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि आने वाले महीनों में कांग्रेस संगठन के चुनाव अगर होते हैं, तो उसमें फिर राहुल गांधी को घेर-घारकर अध्यक्ष बनाया जाए। यह नौबत तब है जब तीन बरस पहले के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने आखिरी बार कोई प्रदेश जीता था, और उसके बाद से वह लगातार हार ही रही है। हार भी छोटी-मोटी हार नहीं है, बहुत बड़ी-बड़ी, ऐतिहासिक, और शर्मनाक हार इस पार्टी ने झेली है। यह पार्टी लंबे समय तक पश्चिम बंगाल पर राज करने वाली पार्टी रही है, और आज हालत यह है कि बंगाल विधानसभा में दूसरी पार्टियों के विधायकों के हाथ की शक्ल में ही कांग्रेस का चुनावी निशान दिख सकता है, इस पार्टी का अपना एक हाथ भी विधानसभा में दाखिल नहीं हो पाया है। करीब-करीब वही हालत उत्तरप्रदेश में भी रही है जहां पर पिछले चुनाव में जीती गई सात सीटें भी अब घटकर दो रह गई हैं। पार्टी 399 सीटों पर लड़ी थी, और भाजपा के 68 फीसदी वोटों के मुकाबले कांग्रेस के वोट एक फीसदी रह गए हैं। जिस प्रदेश से कांग्रेस के एक के बाद एक प्रधानमंत्री रहे हैं, पूरा सोनिया-कुनबा जिस प्रदेश से लड़ते, जीतते, और लड़वाते आया है, वहां पर महज नाम के लिए कांग्रेस विधायक विधानसभा पहुंच पाए हैं। पंजाब में, जैसा कि हमने कल इसी जगह लिखा था, कांग्रेस ने बुरी तरह अपनी सरकार खोई है, और जिस उत्तराखंड और गोवा में एक्जिट पोल उसकी आसपास की संभावनाएं बता रहे थे, वहां भी वह सत्ता पर दावे से कोसों दूर थम गई है। ऐसी हालत में कांग्रेस पार्टी को, और खासकर गांधी परिवार को क्या करना चाहिए?
गांधी परिवार के चाहने वाले, और वफादारों को यह बात सुनने में कुछ कड़वी लग सकती है, लेकिन आज कांग्रेस के एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है कि उसके हित, और सोनिया-परिवार के हित अलग-अलग हो गए हैं। यह पार्टी चाहे तो, और इसी की गुंजाइश भी अधिक है, परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को चाहे तो नाम के लिए ही सही अध्यक्ष बनने का मौका दे सकती है, और अपने परंपरागत पारिवारिक असर को कुछ वक्त के लिए आराम दे सकती है ताकि पार्टी एक नई सोच से दुबारा खड़ी होने की एक कोशिश तो कर सके। नाकामयाबी तो राहुल और सोनिया की लीडरशिप को भी लगातार मिल ही रही है, लेकिन वे पार्टी अध्यक्ष तो बने हुए ही हैं, ऐसे में परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति की लीडरशिप में भी कांग्रेस को अगर नाकामयाबी मिलनी है, तो वह भी मिल जाए, कम से कम यह परिवार अपने आपको कांग्रेस पर काबिज कुनबापरस्त की तोहमत से तो आजाद हो जाएगा। आज जितनी जरूरत कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार की लीडरशिप से परे भी कुछ देखने की है, उतनी ही जरूरत इस परिवार को भी कम से कम कुछ बरस के लिए पार्टी से परे, अध्यक्ष पद से परे कुछ और देखने की है ही। आज इन दोनों को एक-दूसरे से परे राहत की एक सांस की जरूरत है, और एक-दूसरे से परे कुछ संभावनाओं को तलाशने की जरूरत भी है।
आज गांधी परिवार नाकामयाबी की तोहमत तो झेल ही रहा है, वह पार्टी पर किसी भी तरह काबिज रहने पर आमादा रहने की तोहमत भी झेल रहा है। इस सिलसिले के चलते हुए लोग सोनिया गांधी के सारे इतिहास को आसानी से भूल जाते हैं कि किस तरह राजीव गांधी की शहादत के बाद उन्होंने नरसिंह राव को केन्द्र सरकार और संगठन दोनों पर काबिज होने का मौका दिया था, और नरसिंह राव ने बोफोर्स को कुरेदने सहित कई काम किए थे, लेकिन वे सोनिया गांधी को दफन नहीं कर पाए, और आगे चलकर सोनिया की लीडरशिप ने दो बार यूपीए की सरकार बनी, कई राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें बनीं। लेकिन लगातार हार के बाद आज जब खुद राहुल गांधी ने यह साफ किया है कि वे पार्टी अध्यक्ष पद पर न खुद रहेंगे, न परिवार के किसी को रखा जाए, और बाहर के किसी व्यक्ति की लीडरशिप को देखा जाए, तो फिर इस परिवार से अध्यक्ष बनाने, या बनाए रखने का मतलब यह साबित करना है कि राहुल गांधी का तमाम त्याग महज ढकोसला था। यह बात और यह नौबत खुद सोनिया-परिवार के लिए ठीक नहीं है।
यह दौर भारतीय चुनावी राजनीति में बड़ा असामान्य और अस्वाभाविक दौर है जिसमें राहुल और सोनिया सरीखे पार्टटाईम नेताओं का कोई गुजारा नहीं है क्योंकि पूरी तरह नए तौर-तरीकों के साथ मोदी जैसे परिवारविहीन ओवरटाईम करने वाले नेता तस्वीर बदल चुके हैं। इसका मुकाबला संगठन के भीतर परिवार के प्रति निष्ठा के आधार पर नहीं किया जा सकता। आज नए तेवरों, नई सोच, और नई चुनौतियों के साथ पार्टियों को बदले हालात समझने की जरूरत है, उसके बिना किसी की कोई संभावना नहीं बची है। मोदी की अगुवाई में भाजपा ने खेल के नियम पूरी तरह बदल दिए हैं, गोलपोस्ट की जगह बदल दी है, गेंद का आकार बदल दिया है, मैदान की लंबाई-चौड़ाई भी बदल दी है। इन फेरबदल से नावाकिफ लोग किसी मासूमियत का दावा करते हुए बदले तौर-तरीकों की शिकायत नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी से अलग-अलग मौकों पर बहुत से नेताओं ने अलग होकर अपनी अलग कांग्रेस भी बनाई है, और वे दूसरी पार्टियों में भी गए हैं। ऐसी दोनों चीजों का खतरा आज भी कांग्रेस के सामने है, और अगर गांधी परिवार अपने आपको लीडरशिप से अलग नहीं करता है, तो इस नौबत को लाने के लिए भी उसे ही जवाबदेह ठहराया जाएगा।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे अधिक चौंकाने वाले नहीं हैं। दो दिन पहले आए एक्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक ही अभी दोपहर होने तक रूझान चल रहा है, और यह रूझान बदलते नहीं दिख रहा है। मतलब यह कि मतगणना के शुरू के चार घंटों में तस्वीर साफ हो चुकी है, भाजपा अपने सारे राज्य बचाते हुए दिख रही है, और कांग्रेस इन पांच राज्यों में से अपने हाथ का पंजाब बहुत बुरी तरह खोते दिख रही है। इन नतीजों में इन दो बातों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह पंजाब में कांग्रेस, अकाली, भाजपा, सबका सूपड़ा साफ हो गया है, और अकेले आम आदमी पार्टी ने पूरे राज्य में परचम फहरा दिया है। उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड में कुछ नुकसान के साथ ही सही भाजपा सत्ता पर काबिज बनी रहेगी, और अगले पांच बरस यही बात मायने रखती है। अगर मणिपुर, गोवा में भी भाजपा पर्याप्त आगे नहीं रहती, उत्तराखंड में उम्मीद लगाए बैठी कांग्रेस से दुगुने से भी अधिक आगे नहीं रहती, तो उत्तरप्रदेश में सत्ता पर वापिसी की वाहवाही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिस्सेदार होते। लेकिन उत्तरप्रदेश में भाजपा पांच दर्जन से अधिक सीटें खोते दिख रही है, इसलिए वहां योगी के किसी करिश्मे की बात कहना गलत होगा, और चार राज्यों में भाजपा की वापिसी से एक ही बात साबित होती है कि यह मोदी के नाम पर मिला हुआ वोट है। जहां तक पंजाब का सवाल है तो अपनी एक सबसे पुरानी भागीदार अकाली दल से नाता टूटने के बाद वहां भाजपा का यह पहला चुनाव था, और हैरानी की बात यह है कि उसे अकाली दल से थोड़ी ही कम सीटों पर बढ़त दिख रही है। मतलब यह कि अकालियों के खिलाफ लडक़र भी भाजपा पांव जमाए हुए है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो सभी पांच राज्यों में सीटों की शक्ल में उसकी जमीन खिसक जाने, या न जीत पाने के स्पष्ट सुबूत हैं, और अपने बारे में दीवार पर लिक्खी इस हकीकत को कांग्रेस देखना चाहे या नहीं, यह उसकी अपनी पसंद का सवाल है।
इन पांच राज्यों में से सबसे मुश्किल नतीजे पंजाब के होने थे क्योंकि वहां पिछले चुनाव में पैर मजबूती से जमाने के बाद भी जीत से कोसों दूर रहने वाली आम आदमी पार्टी का मुकाबला इस बार कांग्रेस के एक दलित मुख्यमंत्री से था, बसपा के साथ मिलकर लड़ रहे अकालियों से था, भाजपा से था, और किसान उम्मीदवारों से था। राजनीतिक विश्लेषक नौबत को आप के पक्ष में तो मानते थे, लेकिन पांच कोनों में बंटे हुए मुकाबले में नतीजों को लेकर कुछ असमंजस था। लेकिन जैसे-जैसे मतदान हुआ, वैसे-वैसे आप की मजबूत संभावनाएं सामने आ चुकी थीं। अभी दोपहर 12 बजे तक रूझान बताते हैं कि बाकी तमाम पार्टियों को हाशिए पर धकेलकर आम आदमी पार्टी तीन चौथाई बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। देश की राजनीति में शायद आज की तारीख में यह अकेला मामला है जब गैरकांग्रेस, गैरभाजपा कोई पार्टी दो राज्यों में सरकार चलाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अगले आम चुनाव तक किसी विपक्षी गठबंधन में पंजाब की बदौलत एक अधिक वजनदार नेता गिने जाएंगे। पंजाब में कांग्रेस, अकाली, और भाजपा का केजरीवाल ने वही हाल किया है जो कि दिल्ली में किया था।
अब उत्तरप्रदेश की बात करें तो धार्मिक ध्रुवीकरण, जातिगत समीकरण, गरीबों को दिए गए सीधे फायदे जैसी बातें तो थीं, लेकिन इनके साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस बड़े पैमाने पर जितना हमलावर चुनाव प्रचार किया, उससे यह भी कहा जा सकता है कि योगी के नाम पर और मोदी के चेहरे से यह चुनाव जीता गया है। पंजाब की हार भाजपा के लिए बहुत मायने नहीं रखती, क्योंकि वह वहां सत्ता पर भी नहीं थी, उसकी सत्ता पर आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन कांग्रेस के हाथ से एक संपन्न राज्य छिन जाने की नौबत भाजपा के लिए राहत की बात है, और जब भाजपा और कांग्रेस की तुलना होती है तो आज यह संपन्न और विपन्न की तुलना सरीखी है, और जब 2024 के आम चुनाव के लिए जमीन अभी से तैयार हो रही है, तो भाजपा और कांग्रेस के बीच की यह तुलना इन चुनावों से बढक़र मायने रखती है। इन चुनावों के बाद एनडीए के मुकाबले बनने वाले किसी संभावित गठबंधन में कांग्रेस का वजन बहुत कम रह जाएगा, और ऐसी हालत में हो सकता है कि एनडीए के मुकाबले एक के बजाय दो गठबंधनों की नौबत आ जाए, और वह मोदी के लिए 2024 में सबसे सहूलियत की बात होगी।
देश के कोई भी राजनीतिक विश्लेषक इन पांच राज्यों के चुनावों को महज इन्हीं तक सीमित नहीं देख रहे हैं, बल्कि इन्हें 2024 के आम चुनावों के पहले की एक झलक के रूप में भी देख रहे हैं। और जहां तक उत्तरप्रदेश में कांग्रेस को अब तक 403 में से 2 सीटों पर लीड मिलते दिख रही है, पिछले विधानसभा चुनाव से वह 5 सीटें खोते दिख रही हैं, तो ऐसा लगता है कि वहां के वोटरों ने भाजपा गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन के अलावा किसी और को वोट देना वोट खराब करने सरीखा मान लिया था, और बसपा और कांग्रेस दो-तीन सीटों पर आगे हैं जो कि पिछले चुनावों की उनकी सीटों से भी काफी कम हैं। अभी अलग-अलग राज्यों में हासिल वोटों का प्रतिशत सामने आने में कुछ घंटे बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर यह लगती है कि भाजपा ही पंजाब छोड़ बाकी राज्यों में विजेता बनकर उभरी है, और पंजाब में भी उसने अपनी सीटें बढ़ाई हैं, जबकि उसके पुराने भागीदार अकाली दल ने सीटें खोई हैं, और कांग्रेस ने तो पूरी सरकार ही खो दी है।
हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय राजनीति में जिन लोगों को जिंदा रहना है, और प्रासंगिक रहना है, उन्हें हवा-हवाई दावे छोडक़र जमीनी हकीकत को मानना होगा, और मोदी-भाजपा को कम आंकना बंद करना होगा। हमने कल ही इसी जगह पर लिखा था कि मीडिया के जिन लोगों और राजनीति-सामाजिक क्षेत्र के जिन लोगों ने इन राज्यों को लेकर चुनावी भविष्यवाणियां की थीं, वे नतीजे आने के बाद आज शाम अपने उगले हुए शब्दों को सामने रखकर अपनी सफाई दें, राजनीतिक दलों को भी ऐसा करना चाहिए, तभी जाकर वे भविष्य के किसी चुनाव में प्रासंगिक साबित होने की संभावना रख सकेंगे। फिलहाल पूरी तरह से विविधता वाले इन पांच राज्यों में कामयाबी के लिए मोदी और भाजपा बधाई के हकदार हैं, बाकी लोग अपनी-अपनी सजा खुद तय करें, अपना प्रायश्चित खुद तय करें।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का मतदान पूरा हुआ, और उसके तुरंत बाद एक्जिट पोल के नतीजे आने लगे। बहुत से बड़े टीवी चैनलों ने अलग-अलग सर्वे एजेंसियों के साथ मिलकर मतदान के दिनों पर जो सर्वे किया था उसके नतीजे आखिरी मतदान के बाद ही रखे जा सकते थे, और तकरीबन तमाम चैनलों ने अपने और दूसरे चैनलों के सर्वे मिलाकर भी पेश किए। पिछले कुछ दशकों में हिन्दुस्तान में एक्जिट पोल का सिलसिला बढ़ते चले गया है, और कुछ मौकों पर ये अनुमान गलत भी निकले हैं, लेकिन अधिक बार ये सच के करीब रहते हैं। किसी एक चैनल या सर्वे एजेंसी का अनुमान गड़बड़ हो सकता है, लेकिन सभी को मिलाकर अगर देखा जाए, और उनमें नतीजे एक तरफ झुके हुए दिखें, तो मानना चाहिए कि उसी की संभावना अधिक है।
लेकिन एक्जिट पोल से परे पिछले कुछ महीनों से लगातार अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोग अपनी-अपनी पसंद और नापसंद के मुताबिक चुनावी संभावनाओं पर लिख रहे थे। बहुत से अखबार और टीवी चैनल खुलकर किसी पार्टी या नेता के प्रचारक बनकर काम करते आए हैं, और इस बार भी वे उसी किरदार में थे। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले राजनीतिक या सामाजिक चेतनासंपन्न लोग अपनी भावनाओं के मुताबिक भविष्यवाणी करने में लगे हुए थे, और हकीकत का उनका अंदाज उनकी हसरतों से लदा हुआ था। अब दो दिन बाकी हैं, बल्कि कल शाम तक ही तमाम नतीजे सामने आ जाने चाहिए, और दो छोटे राज्यों में कांटे की टक्कर की भविष्यवाणी एक्जिट पोल ने की है, वहां तस्वीर साफ होने में कुछ दिन और लग सकते हैं, लेकिन बाकी जगहों के बारे में कल शाम तक भविष्यवक्ताओं की जवाबदेही तय करने का समय आ जाएगा।
लोकतंत्र में अगर लोग जागरूक नहीं रहते हैं, तो लोग उन्हें बरगला सकते हैं, और हर चुनाव में सिलसिलेवार धोखा दे सकते हैं। लेकिन अगर लोग जागरूक रहेंगे, और अगर वे अखबारों की कतरन सम्हालकर रखेंगे, एक्जिट पोल के स्क्रीनशॉट बचाकर रखेंगे, तो कल उनके हाथ अधिकतर मीडिया के लिए सवाल रहेंगे। लोगों को अखबारों, टीवी चैनलों, वेबसाइटों, और सोशल मीडिया पर लिखने वाले लोगों से जवाब भी लेने चाहिए। कल शाम जब राज्यों की तस्वीर साफ हो जाएगी, और एक-एक विधानसभा सीट पर जीत-हार और लीड का आंकड़ा सामने रहेगा, तो लोगों को अपने-अपने इलाके, प्रदेश, या पूरे देश की भविष्यवाणी करने वाले लोगों से उनका अनुमान गलत होने पर जवाब मांगना चाहिए, या कम से कम उनकी भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर याद दिलानी चाहिए। अगर हर किसी के पाठक, श्रोता, और दर्शक ऐसा करने लगेंगे, तो अगली बार अपनी कलम या आत्मा बेचकर झूठी भविष्यवाणई करने वाले लोग भी कुछ शर्म महसूस करेंगे, और जिन लोगों ने बिना कुछ बेचे सिर्फ अपनी हसरतों को हकीकत लिखा था, वे लोग भी अगली बार अधिक सावधान होने को मजबूर रहेंगे। लोग कुछ भी लिख देते हैं, और कुछ भी बोल देते हैं, और इसके बाद भी कोई उनसे जवाब नहीं मांगते, तो यह गैरजिम्मेदारी को बढ़ाने का सिलसिला रहता है। एक जिम्मेदार लोकतंत्र के नागरिकों को ऐसे सिलसिले के खिलाफ सवाल उठाने चाहिए।
दुनिया भर में कहीं भी कोई ओपिनियन पोल हो, या एक्जिट पोल हो, इन सब का सौ फीसदी सही होना जरूरी नहीं होता, लेकिन उसके पीछे अगर कोई बदनीयत है, तो उसका उजागर होना जरूरी होता है। फिर अगर बिना बदनीयत के भी कुछ लोग अपने नाम की शोहरत को भुनाते हुए किसी नेता या पार्टी, या गठबंधन की जीत या हार के बड़े-बड़े दावे करते हैं, तो उनकी कही बातों के स्क्रीनशॉट के साथ नतीजों को रखना चाहिए ताकि अगली बार झूठे या गैरजिम्मेदार दावे करते हुए वे उजागर हो सकें, लोग उन्हें उनके पिछले दावों और उनके बाद के नतीजों की याद दिला सकें। लोगों को आज कम्प्यूटर और मोबाइल फोन की मेहरबानी से रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, और समाचारों के लिंक बचाकर रखना आसान हो गया है। हिन्दुस्तान में ही दुनिया के कुछ और विकसित लोकतंत्रों की तरह फैक्ट-चेक करने वाली वेबसाइटें काम करती हैं, और ऐसी कोई वेबसाइट भी लोगों के दावों और नतीजों को अगल-बगल रखकर आम पाठकों या दर्शकों के राजनीतिक शिक्षण का काम कर सकती हैं। लोकतंत्र में जनता की राजनीतिक चेतना का विकास जरूरी रहता है, और आज झूठ का कारोबार इतना जोर पकड़ चुका है कि लोग अपने पूर्वाग्रहों को माकूल बैठने वाले झूठ को बढ़ाने के काम में लगे रहते हैं, और सच मानो रोजगार दफ्तर के बाहर निराश बैठे बेरोजगार की तरह रहता है। ऐसे में जिम्मेदार तबकों को दावों की हकीकत सामने रखना चाहिए, इनमें चुनावी भाषणों के झूठ तो बीच-बीच में लोग उजागर करते रहते हैं, लेकिन अपने आपको तटस्थ बताने वाला लेकिन बिक चुका मीडिया जिस तरह किसी उम्मीदवार या पार्टी को जिताने में लगे रहता है, उसके दावों को भी नतीजों के साथ मिलाकर लिखा जाना चाहिए ताकि वैसे मीडिया की आने वाले बरसों में साख तय हो सके।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
पाकिस्तान सरहद के करीब हिन्दुस्तान के अमृतसर में बीएसएफ के मुख्यालय में एक जवान ने अपने साथियों पर गोलियां चला दीं जिनमें चार लोग मारे गए, और बाद में इसी गोलीबारी में वह जवान खुद की या किसी और की गोली से मारा गया। सशस्त्र बलों के बीच हिन्दुस्तान में हर बरस ऐसी कई वारदातें होती हैं, और ऐसी तनावपूर्ण हिंसा का निशाना साथी ही बनते हैं। हर बरस छत्तीसगढ़ के बस्तर के नक्सल मोर्चे पर तैनात सशस्त्र बलों के बीच ऐसी हिंसा सामने आती है, और जांच के बाद जिंदा बचे हमलावर पर शायद कोई कार्रवाई होती हो, लेकिन यह बात सामने नहीं आती कि अपने जवानों में हिंसा की इस हद तक ले जाने वाले तनाव का क्या समाधान सुरक्षा बल निकालते हैं। हर बार यह बात तो मंजूर कर ली जाती है कि गोलियां चलाने वाला जवान तनाव में था, यह भी होता है कि साथी जवान खिल्ली उड़ाते हैं जिससे भडक़कर कोई जवान गोलियां चला देता है। बहुत से मामले लगातार मुश्किल ड्यूटी से थके हुए जवानों की हिंसा के रहते हैं, और कई मामलों में घर जाने की छुट्टी न मिलने पर अपने से सीनियर से हुए तनाव के बाद जवान ऐसे हमलावर हो जाते हैं।
हिन्दुस्तान के न सिर्फ सशस्त्र सुरक्षा बलों में, बल्कि राज्यों की पुलिस में भी जवानों से नाजायज मुश्किल ड्यूटी ली जाती है, न आराम का वक्त दिया जाता, न सम्मान का काम दिया जाता। नतीजा यह होता है कि इनके भीतर तनाव बढ़ते चलता है। वक्त-जरूरत परिवार के पास न जा पाना तनाव की एक वजह रहती है, लेकिन दूसरी वजह यह भी रहती है कि परिवार की उपेक्षा होते चलने से वहां दिक्कतें खड़ी होती हैं, और फोन पर उसकी जानकारी और तनाव खड़ा करती है। लोगों को याद होगा कि पिछली भाजपा सरकार के समय से छत्तीसगढ़ में पुलिस जवान और उनके परिवार साप्ताहिक छुट्टी की मांग कर रहे थे, और पुलिस परिवारों ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया था। वह आंदोलन अभी तक जारी है, और कुछ हफ्ते पहले उसमें लगे हुए लोगों पर बड़े संगीन जुर्म दर्ज किए गए हैं। जुर्म दर्ज करना तो सरकार के हाथ में होता है लेकिन कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा कर पाना उसके मुकाबले बड़ा अधिक मुश्किल काम रहता है।
सत्ता पर बैठे हुए जो लोग हथियारबंद जवानों में फैले हुए तनाव को लेकर कोई फिक्र जरूरी नहीं समझते, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि नेताओं की हिफाजत में भी यही लोग लगे रहते हैं, और किसी दिन उनकी बेकाबू हिंसा का निशाना कोई सत्तारूढ़ नेता भी बन सकते हैं। इसलिए और किसी वजह से न सही तो कम से कम अपनी हिफाजत के लिए नेताओं को सुरक्षा बलों और पुलिस के तनाव दूर करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। सुरक्षाकर्मी और पुलिस इसी देश के नागरिक रहते हैं, और अपनी-अपनी सरकारों, या अपने अफसरों-नेताओं के भ्रष्टाचार के किस्से भी पढ़ते रहते हैं। इसलिए उनके मन में इस बात को लेकर भी रंज रहता है कि उन्हें भ्रष्ट लोगों के मातहत, उनके लिए काम करना होता है। ऐसे में उनसे अतिरिक्त निष्ठा की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। बड़े अफसरों के बंगलों पर बच्चों से लेकर कुत्तों तक को खिलाने के लिए मातहत कर्मचारियों का बेजा इस्तेमाल हिन्दुस्तान में हर कहीं देखने मिलता है। ऐसी बंगला-ड्यूटी के खिलाफ भी सरकारों को सोचना चाहिए क्योंकि घरेलू नौकरों के करने वाले काम पर जब बहुत अधिक तनख्वाह वाले पुलिस और सुरक्षा कर्मचारियों को झोंक दिया जाता है तो यह बात उनके मनोबल को भी तोड़ती है, और सरकार के खर्च की बड़ी बर्बादी होती है।
आज का वक्त हर मोबाइल फोन पर वीडियो-कैमरे का है, और लोगों को चाहिए कि जहां कहीं किसी नेता-अफसर के घर कर्मचारियों का ऐसा इस्तेमाल होता है, उसकी रिकॉर्डिंग करके उसे उजागर करना चाहिए। साथ ही जनसंगठनों को या ऐसे जवानों के परिवारों को जनहित याचिका लेकर अदालत भी जाना चाहिए ताकि वर्दीधारी जवानों से स्तरहीन निजी काम करवाना बंद हो सके।
आज की बात जहां से शुरू हुई थी उस पर अगर लौटें तो सशस्त्र बलों को अपने जवानों को छुट्टी देने और उनके परिवार का ख्याल रखने के बारे में सोचना चाहिए। परिवार से बहुत लंबे समय तक दूर रहने वाले जवानों का तनाव बहुत बढ़ा हुआ रहता है, और हिंसा की खबरों से नीचे भी यह तनाव कई अलग-अलग स्तरों पर रहता है जिससे जवानों को निजी नुकसान भी होता है, और ऐसी फोर्स भी कमजोर होती है। यह बात अक्सर उठती है कि जवानों में तनाव घटाने के लिए सशस्त्र बलों में परामर्शदाता या मनोचिकित्सक रखे जाएं, लेकिन शायद वैसा हो नहीं पाता है क्योंकि मनोचिकित्सकों की देश में भारी कमी है। फिर भी जहां हथियारबंद रहना ही काम का हिस्सा हो, वहां पर लोगों का तनावग्रस्त रहना सभी के लिए जानलेवा हो सकता है। बिना देर किए इस नौबत को सुधारना चाहिए।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जानवरों के कुछ दिलचस्प वीडियो देखें तो लगता है कि किस तरह वे एक दूसरे की जिंदगी बचाने के काम आते हैं। कहीं कोई कुतिया बिल्ली के बच्चों को दूध पिलाकर बचा रही है, तो आज ही एक वीडियो ऐसा पोस्ट हुआ है जिसमें पानी में डूब रही गिलहरी को बचाने के लिए एक कुत्ता पानी में कूदा, और उसे अपने सिर पर बिठाकर किनारे ले आया। इंसान को छोडक़र धरती, पानी और आसमान के कोई भी जीव-जंतु इंसान जितना सोचने वाले नहीं होते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन जब पशु-पक्षियों के बीच इस तरह की आपसी हमदर्दी दिखती है तो लगता है कि इंसानों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पशु-पक्षियों से कुछ सीखने की जरूरत है। ऐसे तो हम पहले भी यह बात लिखते आए हैं कि लोगों को कुदरत से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए, और दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग जंगल और पेड़ों तक जाकर, उनके बीच कुछ वक्त गुजारकर अपने-आपको बेहतर बनाते हैं। जिन जानवरों का इस्तेमाल इंसान आमतौर पर गालियां बनाने के लिए करते हैं, और अपने बीच के घटिया लोगों को कोसने के लिए जानवरों की मिसालें देते हैं, उन इंसानों को यह सोचना चाहिए कि जानवरों में भला इंसानों जितने मतलबपरस्त कहां होते हैं?
जब इंसान तनाव में रहें, तो शायद बच्चों और पशु-पक्षियों के वीडियो देखने पर वह तनाव कम होता है। और फिर अब तो हर हाथ में एक वीडियो कैमरा होने से जानवरों और बच्चों के दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही रहते हैं, और वे लोगों का तनाव घटाने में मददगार होते हैं। कहीं कोई पक्षी पानी के किनारे बैठकर सतह पर आने वाली मछलियों के मुंह में खाना देते जा रहा है, कहीं कोई कुत्ता किसी बिल्ली को लिपटाकर सुला रहा है, ऐसे अनगिनत वीडियो आते हैं और इन्हें देखकर इंसानों को यह सोचना चाहिए कि एक ही इंसानी बिरादरी के होने के बावजूद उनके बीच किस हद तक नफरत फैली हुई है, रंग, जाति, और धर्म इन सबका कितना तनाव भरा हुआ है, जिंदगी की बुनियादी बातों को छोडक़र बाकी बातों के लिए किस हद तक हिंसा हो रही है। इंसान तो जानवरों के मुकाबले अधिक बड़ा दिमाग रखते हैं, पढ़े-लिखे हैं, उन्हें धर्म और आध्यात्म जैसी आस्था का भी सहारा है, लेकिन वे हिंसा के मामले में जानवरों से अधिक हिंसक हैं। कुदरत ने जिस जानवर को जैसे खानपान का बनाया है, उससे परे वे कुछ नहीं खाते। जो मांसाहारी भी हैं, वे भी शायद अपनी नस्ल को नहीं खाते, और जिन दूसरे प्राणियों को वे मारते हैं, उन्हें भी महज अपनी भूख की जरूरत के लिए मारते हैं, मार-मारकर अपना गोदाम भरकर नहीं रखते। इंसानों के मुकाबले जानवरों को देखें तो अधिकतर नस्लों में नर मादा को रिझाने के लिए तरह-तरह से कोशिश करते हैं, उसका दिल जीतने की कोशिश करते हैं, दूसरे नर प्राणियों को हराकर मादा को जीतते हैं। मतलब यह कि इंसानों के बीच जिस तरह का लैंगिक भेदभाव हिंसा तक पहुंचा हुआ रहता है, वैसा जानवरों के बीच कहीं भी नहीं दिखता।
आज जब सोशल मीडिया पर नफरत और हिंसा को फैलाने का काम कुछ लोग पूरी निष्ठा और भक्ति-भाव से एक मजदूरी या समर्पण की तरह करते हैं, तब कुछ लोग जानवरों और बच्चों के आपसी प्रेम के वीडियो भी डालते हैं जिनमें कोई कुत्ता या कोई बिल्ली किसी इंसानी बच्चे को अपने में समेटकर हिफाजत से रखते हैं, और बच्चे भी उनके साथ सबसे अधिक आराम से रहते हैं। ऐसे वीडियो देखकर दूसरे प्राणियों को तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे इंसानी नफरत से अब तक अछूते हैं, लेकिन इंसानों को इनसे यह सीखना चाहिए कि किस तरह दूसरे प्राणी इंसानों के बच्चों को भी इतनी मोहब्बत से साथ रखते हैं। आज अगर लोगों को अपना खासा वक्त कम्प्यूटर या मोबाइल फोन पर गुजारना ही है, तो भी उन्हें नफरत की बातों के बजाय मोहब्बत की बातें सीखने के लिए पशु-पक्षियों और मछलियों के ऐसे वीडियो देखना चाहिए जो कि इंसानों से बेहतर खूबियों वाले प्राणी दिखाते हैं। आज घर-घर में बच्चे कार्टून फिल्में देखते हैं, और वीडियो गेम खेलते हैं। उनका स्क्रीन-टाईम अगर कम करना मुमकिन नहीं है, तो भी हमारा यह मानना है कि उन्हें बच्चों और जानवरों के ऐसे वीडियो दिखाए जाएं जो कि बेहतर प्रकृति दिखाते हैं, बेहतर खूबियां दिखाते हैं। बचपन से ही अगर बच्चे अपना कुछ समय सहअस्तित्व की ऐसी बातों को देखते हुए गुजारते हैं, तो उनके मन में दूसरे प्राणियों के लिए भी सम्मान रहेगा, और दूसरे लोगों के लिए भी।
दुनिया के बहुत से देशों में, बहुत सी संस्कृतियों में इंसानी जिंदगी में भी प्रकृति के महत्व को लंबे समय से गिनाया गया है। लोगों को अपने परिवार सहित जब मुमकिन हो तब कुदरत के बीच जाना चाहिए, और शहरी फोन-कम्प्यूटर को जितने वक्त अलग रख सकें, अलग रखकर प्रकृति के बीच जीकर देखना चाहिए। कुदरत से बड़े कोई शिक्षक नहीं हो सकते, और उसके हर पहलू से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। पशु-पक्षी इसी कुदरत का एक हिस्सा हैं, और सोशल मीडिया पर अगर आए दिन उनके खूबसूरत मिजाज को दिखाने वाले वीडियो पोस्ट करने वाले लोगों को फॉलो किया जाए, तो इंसान खुद भी अपने तनाव से बच सकते हैं, वे एक बेहतर इंसान बन सकते हैं।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
हिन्दुस्तानी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उस भाजपा के नेता हैं जो कि विदेश नीति के मामले में अमरीका के अधिक करीब मानी जाती है। इसकी वजह भी बहुत साफ है कि सोवियत संघ के वक्त से लेकर आज के रूस के वक्त तक रूसी नीतियां भारत में वामपंथी दलों के करीब है, दूसरी तरफ चीन के साथ सरहदी टकराव और ऐतिहासिक जंग के तजुर्बे से परे भी भारत का एक वामपंथी दल चीन की नीतियों के करीब माना जाता है, और इसलिए भाजपा का इन दोनों देशों से परहेज समझ आता है। इसलिए जब नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अमरीका से अपने रिश्ते मजबूत रखे तो वह कोई हैरानी की बात नहीं थी। बाद के बरसों में वे जिस तरह पिछले अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प के करीब हो गए, और दोनों ने एक-दूसरे का चुनाव प्रचार किया, तो ऐसा लगने लगा था कि भारत अब अमरीकी कैम्प में है। लेकिन जटिल अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में न तो कोई स्थाई दोस्त होते हैं, और न ही स्थाई दुश्मन। यह जरूर हुआ है कि हर आड़े वक्त हिन्दुस्तान के साथ खड़े रहने वाला रूस आज जब यूक्रेन पर हमला करके पश्चिमी दुनिया और योरप का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है, तब भारत ने रूस का साथ देना तय किया है, या कम से कम रूस का विरोध नहीं किया है। इससे एक ही बात साबित होती है कि देश के हित किसी पार्टी या नेता के निजी हितों से ऊपर रहते हैं, और मोदी की आज की रूस-यूक्रेन नीति देश की नीति की तरह है, और भारत के विपक्षी राजनीतिक दल भी इस मोर्चे पर सरकार से सहमत दिख रहे हैं। आज अगर भारत का विपक्ष सरकार की आलोचना कर रहा है तो वह यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापिसी को लेकर है, न कि सरकार की विदेश नीति को लेकर।
सरकार की नीतियों से प्रत्यक्ष रूप से न जुड़े हुए स्वतंत्र विचारक रूस के ऐसे हमले के खिलाफ भी हैं। लेकिन यह तो लोकतांत्रिक आजादी है जो कि लोगों को अपने देशहित से ऊपर विश्वहित में सोचने का मौका देती है, सोचने को मजबूर करती है। नक्शे की सरहदी लकीरों को नजरअंदाज करते हुए जो लोग सोच पाते हैं, वे ही लोग किसी एक देश के नागरिक से ऊपर का दर्जा पाते हैं। सरकारों के सामने तो यह मजबूरी रहती है कि उन्हें सबसे पहले अपने देश के भले के बारे मेें सोचना पड़ता है, अपने देश की हिफाजत करनी पड़ती है। लेकिन स्वतंत्र सोच रखने वाले लोग इससे ऊपर की बात भी सोचते हैं और करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि किसी देश का नेता रहते हुए, शासन प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख रहते हुए दुनिया के कुछ नेताओं ने अपने देश के हित से ऊपर उठकर कुछ न किया हो। यहीं पर आकर यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति अपने देश के शासन प्रमुख हैं, या कि वे विश्व के नेता हैं। कभी-कभी व्यापक अंतरराष्ट्रीय हित के लिए अपने सीमित राष्ट्रीय हितों को कुछ हद तक कुर्बान भी करना पड़ता है, और दुनिया के महान नेताओं ने ऐसी दुविधा की नौबत आने पर विश्वहित को ऊपर रखकर फैसले लिए हैं, पहल की है, और इतिहास में न सिर्फ अपनी बल्कि अपने देश की एक अलग जगह बनाई है।
अब सीरिया, इराक, या अफगानिस्तान जैसे देशों से योरप पहुंचने वाले शरणार्थियों की बात देखें तो पश्चिम के विकसित देशों ने अपने देश के लिए आर्थिक बोझ, समस्याएं, और कुछ हद तक खतरा भी खड़ा करके शरणार्थियों को जगह दी, और अपनी वैश्विक जिम्मेदारी पूरी की। आज भी जब यूक्रेन से दसियों लाख लोगों के शरणार्थी होकर दूसरे देशों में जाने की खबर है तब भी योरप के दूसरे देश इस ऐतिहासिक चुनौती के मौके पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए डटे हुए हैं। दुनिया का इतिहास तंगनजरिए और तंगदिली को तारीफ के साथ दर्ज नहीं करता, बल्कि उन देशों के बड़प्पन को दर्ज करता है जो कि आसपास या दूर-दूर के देशों से आने वाले शरणार्थियों की मदद करते हैं। जब योरप से दूर बचे हुए देशों से लाखों मुस्लिम शरणार्थी समंदर पार करके बोट से यूरोपीय देश पहुंचे, तो स्थानीय सामाजिक असमंजस के बीच भी सरकारों ने लाखों लोगों को जगह दी। ऐसे में हिन्दुस्तान के उन लोगों को अपने बारे में सोचना चाहिए जिन्हें म्यांमार से जान बचाकर आए हुए रोहिंग्या शरणार्थियों की मौजूदगी आंख की किरकिरी की तरह खटक रही है।
आज जब दुनिया की सारी घोषित महाशक्तियां रूस के हमले पर खेमों में बंटी हुई हैं, तो यूक्रेन से लेकर रूस तक हर एक ने भारत की तरफ देखा, और भारत के साथ की अपील की, उम्मीद की। अब तक हिन्दुस्तान का रूख कूटनीतिक रूप से संयुक्त राष्ट्र में रूस की मदद करता हुआ दिखा, और हिन्दुस्तान ने रूस के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन क्या अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के अलावा, रूस के हमले की आलोचना से परहेज करते हुए भी भारत के पास यह विकल्प था, कि वह ऐसे हमले में लोगों की मौत रोकने के लिए इन दोनों देशों के बीच किसी किस्म की मध्यस्थता कर सकता था? या उसका ऐसा कोई वजन नहीं है कि कोई उसकी बात सुनते? ऐसे ही वक्त देश के नेताओं का अंतरराष्ट्रीय महत्व पता चलता है कि वे अपने से सीधे-सीधे न जुड़े हुए लेकिन विश्व शांति के मुद्दे पर किस किस्म की भूमिका निभा सकते हैं। यह मौका अपने देश और अपने वोटरों से ऊपर उठकर विश्व इतिहास में अपने देश की भूमिका दर्ज करवाने का भी रहता है, और आज के दुनिया के तमाम तटस्थ बने हुए देशों के लोगों को अपने देश और अपने नेता की भूमिका के बारे में भी सोचना चाहिए। दुनिया का इतिहास सरहदों के आरपार असर रखने वाले कई नेताओं के ऐतिहासिक वैश्विक योगदान से भरा हुआ है। हम यहां पर किसी की किसी से तुलना करना नहीं चाहते, लोग खुद ही यह काम कर सकते हैं। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि यूक्रेन से अपने लोगों को बचाने के अलावा भी हिन्दुस्तान की एक भूमिका जंग के इस मोर्चे पर रहनी चाहिए थी, जो कि आज नजर नहीं आ रही है। राष्ट्रहित के सीमित नजरिये से ऐसी तटस्थता को जायज ठहराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन इतिहास में अपनी जगह तय करना खुद के हाथ में नहीं होता है, इतिहास आत्मकथा नहीं होती है, उसे दूसरे लोग लिखते हैं।
यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूक्रेन की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक-एक करके अलग-अलग शहर तबाह हुए चले जा रहे हैं, और पूरी दुनिया की फिक्र खड़ी करने के लिए यूक्रेन के परमाणु बिजलीघर और परमाणु ठिकानों की खबरें आ रही हैं जिन पर रूसी फौजें कब्जा करने की तरफ हैं। इन सबसे परे हिन्दुस्तान जैसे देश की एक सामाजिक परेशानी यह है कि यहां के दसियों हजार छात्र-छात्राओं की पढ़ाई यूक्रेन में चल रही है, और इस जंग के चलते जान बचाकर वे सब हिन्दुस्तान लाए जा रहे हैं। अभी तो उनकी वापिसी का काम भी किसी किनारे नहीं पहुंचा है, चल ही रहा है, लेकिन एक दूसरी दिक्कत जो सामने है वह यह कि इनकी आगे की पढ़ाई का क्या होगा?
यूक्रेन में पढऩे वाले भारतीय छात्र-छात्राओं में हजारों ऐसे हैं जो कि वहां मेडिकल पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। अब यह पढ़ाई न तो किस्तों में हो सकती है, न ही बाकी की पढ़ाई किसी और देश में हो सकती है। यूक्रेन का ढांचा रूसी हमले में तबाह होते दिख रहा है, और आगे भी वहां का माहौल कितना महफूज रह सकेगा, इसे लेकर भी शक है। एक खतरा यह भी है कि यूक्रेन का कुछ हिस्सा वहां की सरकार के काबू से बाहर चले जाए, या पूरे के पूरे यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाए। ऐसा अगर नहीं भी होता है, और यूक्रेन की मौजूदा सरकार पूरे देश पर काबिज रहती है, तो भी रूस की सरहद के करीबी शहरों में पढ़ हिन्दुस्तानी छात्र-छात्राओं का वहां लौटना खतरे से भरा हुआ रहेगा। ऐसे में उनकी आगे की पढ़ाई का क्या होगा? वे अपने पैसों से और अपनी मर्जी से पढऩे विदेश गए थे, इसलिए भारत सरकार की उनकी पढ़ाई को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, लेकिन ऐसे बच्चों पर आई समस्या भारत के एक तबके पर आई हुई समस्या तो है ही।
लेकिन इन 20-25 हजार छात्र-छात्राओं के मुद्दे को कुछ देर के लिए छोड़ भी दें, तो भी एक दूसरा बड़ा मुद्दा यह बचा रह जाता है कि भारत इतना बड़ा देश होने के बाद भी, और यहां के गांव-गांव तक डॉक्टरों की कमी होने के बाद भी यहां मेडिकल कॉलेज काफी क्यों नहीं हैं? यूक्रेन जैसे परदेस में जाकर हिन्दुस्तानी छात्र-छात्राओं को पढ़ाई करनी पड़ती है क्योंकि हिन्दुस्तान के मेडिकल कॉलेजों में एक-एक सीट के लिए कड़ा मुकाबला रहता है, और निजी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए करोड़ों रूपए देने पड़ते हैं। यह नौबत नई नहीं है, लंबे समय से चली आ रही है, और आम जनता के लिए डॉक्टरों की कमी है, छात्र-छात्राओं के लिए मेडिकल सीटों की कमी है, और जो मेडिकल कॉलेज हैं भी वे नामौजूद प्राध्यापकों के कागज लगाकर किसी तरह इंडियन मेडिकल कौंसिल की कागजी खानापूरी करते हैं, और इसी धोखाधड़ी के लिए इस कौंसिल के लोग भारी भ्रष्टाचार से घिरे हुए पकड़ाए भी जा चुके हैं। तो एक तरफ तो नए मेडिकल कॉलेज खुलने के लिए मान्यता पाने को खासी मोटी रिश्वत देने की लंबी परंपरा रही है, और फिर प्राध्यपकों की जरूरत पूरी करने के लिए कागज लगाकर, अस्पताल की औपचारिकता पूरी करने के लिए फर्जी मरीज भर्ती करके मेडिकल कौंसिल की विजिट की औपचारिकता पूरी की जाती है। जाहिर है कि ऐसी पढ़ाई भी कोई बहुत अच्छे डॉक्टर तैयार नहीं कर सकती, और निजी मेडिकल कॉलेजों का तो पूरा ढांचा ही बड़े भ्रष्टाचार का अड्डा रहते आया है।
अभी समस्या आई तो यूक्रेन से है, और वहां पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र-छात्राओं की है, लेकिन ऐसे मौके पर भारत सरकार और प्रदेशों की सरकारों को मिलकर या फिर अलग-अलग भी यह देखना चाहिए कि किस तरह हिन्दुस्तान में मेडिकल कॉलेज बेहतर हो सकते हैं, किस तरह उनमें सीटें बढ़ सकती हैं, या कैसे नए मेडिकल कॉलेज शुरू हो सकते हैं? ऐसे सारे सवालों के जवाब ढूंढने का यह सही वक्त है क्योंकि यह समस्या न सिर्फ डॉक्टर बनने की चाहत रखने वाले बच्चों की है बल्कि यह गरीब भारतीय मजदूरों की भी समस्या है जिन्हें डॉक्टर नसीब नहीं होते हैं।
हिन्दुस्तान का पूरा मेडिकल ढांचा कल्पनाशीलता और योजना की कमी का शिकार है। और यह बात महज पिछले सात बरस की मोदी सरकार के वक्त हुई हो ऐसा भी नहीं है, और यह बात सिर्फ केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी हो ऐसा भी नहीं है। हिन्दुस्तान में निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों का ढांचा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग क्षमता का है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में सभी तरह की उच्च शिक्षा का ढांचा बाकी हिन्दुस्तान से बेहतर बनाकर रखा है। चाहे कैपिटेशन फीस देकर ही इन राज्यों के निजी कॉलेजों में दाखिला होता हो, वह पैसा हिन्दुस्तान में ही कम से कम कुछ हद तक तो खर्च होता है, और वहां पढ़े हुए, डॉक्टर बने हुए लोग यहां काम करने की संभावना रखते हैं। लेकिन यूक्रेन जैसी जगह जाकर डॉक्टरी पढऩे वाले लोग पता नहीं हिन्दुस्तान के गांवों में जाकर काम करना कभी चाहेंगे या नहीं। इसलिए आज यूक्रेन-संकट के मौके पर भारत सरकार को सभी राज्यों के साथ बात करके यह देखना चाहिए कि किस तरह मेडिकल कॉलेज, मेडिकल सीटें, इन कॉलेजों से जुड़े हुए अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज बढ़ाए जा सकते हैं? क्योंकि इस क्षमता को बढ़ाने में जितनी देर होगी, उतनी ही देर से हिन्दुस्तानी मरीजों को डॉक्टर मिल सकेंगे। हम मेडिकल पढ़ाई के स्तर को गिराए बिना इसकी सीटें बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं जिनके लिए हो सकता है कि निजी प्रैक्टिस में मोटी रकम कमाने वाले डॉक्टरों को भी खासी अधिक तनख्वाह देकर लाना पड़े। लेकिन यह काम जरूरी है, और इस बारे में बिना देर किए राज्यों को भी अपने-अपने स्तर पर सोचना चाहिए।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
भारत में पिछले कुछ महीनों से एक नए किस्म का कारोबार जोर पकड़ रहा है जिसे क्विक कॉमर्स कहते हैं, मतलब यह कि सामान की तुरंत बिक्री-डिलीवरी। कुछ ऐसी कंपनियों ने काम शुरू किया है जो 10 से 15 मिनट में किराने का सामान घर पर पहुंचाने का दावा करती हैं, और यह बाजार पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा है। जिन आंकड़ों का कोई अधिक मतलब हम नहीं समझते हैं उन आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान में किराना बाजार करीब 600 अरब डॉलर का है, और मोबाइल फोन पर किए गए ऑर्डर से 10-15 मिनट में घर पर सामान पहुंचाने वाली क्विक कॉमर्स कंपनियों का कारोबार 2025 तक 15 गुना बढक़र 5.5 बिलियन डॉलर होने की एक रिपोर्ट आई है। इन आंकड़ों से आम लोग कोई अधिक अंदाज नहीं लगा सकते, लेकिन बाजार के जो तौर-तरीके बदल रहे हैं उन्हें लेकर हम अपने आसपास के मोहल्ले और कॉलोनी के छोटे-छोटे किराना दुकानदारों की जिंदगी बदल जाने, या अधिक सही यह कहना होगा कि तबाह हो जाने की तस्वीर का अंदाज जरूर लगा सकते हैं।
हिंदुस्तान के बड़े और मंझले आकार के शहरों में पहले से ही बड़े-बड़े सुपर बाजार खुले हैं, जहां से लोग कुछ रियायती दाम पर महीने भर का सामान एक साथ ले आते हैं और पड़ोस की किराना दुकान का काम वैसे भी पिछले वर्षों में तेजी से घटते गया है। अब उन बड़े बाजारों के मुकाबले भी 10 मिनट में घर पर सामान पहुंचाने वाली इन क्विक कॉमर्स कंपनियों के बीच भी कड़ा मुकाबला चल रहा है, और ऐसी खबरें हैं कि रिलायंस और अमेजॉन जैसी कुछ सबसे बड़ी कंपनियां भी सुपर बाजार के बाद अब इस धंधे में भी उतरना चाह रही हैं. एक ग्राहक के लिए यह बड़ी तसल्ली की बात हो सकती है कि आधा किलो नमक का उसका पैकेट अंबानी की कंपनी से घर पर पहुंचा है। जंगल की आग की रफ्तार से यह कारोबार तो आगे बढ़ सकता है, क्या इस रफ्तार से आज के किराना व्यापारी अपने लिए किसी नए काम-धंधे की सोच सकते हैं?
यह तस्वीर बहुत भयानक है। बहुत से किराना व्यापारी तो दूसरी और तीसरी पीढ़ी के भी हैं जो उसी जगह पर काम करते आए हैं, और जो मोहल्ले के लोगों का हिसाब एक कॉपी में दर्ज करके उन्हें सामान देते रहते हैं और फिर महीने में उसका भुगतान पाते हैं। लेकिन उनके लिए भी यह मुमकिन नहीं होगा कि वह ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन बनाएं और लोगों को घर तक सामान पहुंचाएं। अगर मान लीजिए ऐसा हो भी जाता है, तो भी उनके लिए यह मुश्किल होगा इस धंधे में उतरी हुई बड़ी कंपनियों जितना स्टॉक रख सकें और अलग-अलग सामान ग्राहक के लिए मोबाइल ऐप पर पेश कर सकें। तो ऐसे में हिंदुस्तान के करोड़ों मोहल्ला दुकानदारों के सामने एक बड़ा खतरा खड़ा हुआ दिखता है जिससे निपटने के लिए उन्हें तैयारी करनी होगी ।
ऐसा भी नहीं है कि यह नौबत पहली बार आ रही है। लोगों को याद होगा कि जब एसटीडी पीसीओ चलते थे और लोग वहां जाकर दूसरे शहरों में फोन लगाते थे तो हर चौराहों के आसपास ऐसे पीसीओ दिखते थे और इनमें दो-दो तीन-तीन लोगों को काम भी मिल जाता था, कम तनख्वाह का काम, लेकिन रोजगार तो रोजगार ही रहता है। मोबाइल फोन आया और रातों-रात ये सारे पीसीओ बंद होने लगे। लेकिन दूसरी तरफ मोबाइल फोन की बिक्री, उससे जुड़े हुए दूसरे सामानों की बिक्री, और उसकी मरम्मत जैसे काम के लिए, मोबाइल कंपनियों के सिम कार्ड बेचने के लिए इन्हीं या ऐसी ही जगहों पर यही लोग या कुछ दूसरे लोगों को कारोबार और रोजगार मिल गया। कुछ बरस के भीतर ही जितने एसटीडी पीसीओ थे, उससे 10 गुना अधिक मोबाइल और सिम कार्ड की दुकानें खुल गईं। नौकरियां खत्म नहीं हुई, उनकी शक्ल बदल गई, कारोबार भी पूरी तरह से तबाह नहीं हुए, लोगों को दूसरे कारोबार करना पड़ा। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब जब छोटे-छोटे से काम में दुनिया की सबसे बड़ी-बड़ी कंपनियां उतर रही हैं और वे बाजार के मुकाबले में पहले ग्राहकों को अंधाधुंध सहूलियतें और रियायतें देने जा रही हैं, तो हिंदुस्तान की आज की उदार अर्थव्यवस्था को यह भी सोचना पड़ेगा कि क्या सचमुच यह देश इतने अधिक कारोबारी बदलाव के लिए तैयार है? या फिर छोटे छोटे दुकानदारों का धंधा छीनकर बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों या हिंदुस्तान के सबसे बड़े कारोबारियों की जेब में चले जाए तो उससे हिंदुस्तान की सरकार के जीडीपी पर कोई फर्क नहीं पड़ता?
ग्राहकों की जरूरतें तो बनी रहेंगी और मोबाइल फोन पर एक बार छूकर सामान बुलाने की सहूलियत उनकी खरीदारी को बढ़ाएगी ही, इसलिए सरकार को तो असंगठित छोटे कारोबारियों के मुकाबले संगठित बड़े कारोबारियों से मिलने वाला टैक्स कहीं भी कम नहीं होगा और देश की अर्थव्यवस्था के कुल जमा आंकड़ों में बहुत नुकसान नहीं दिखेगा, और हो सकता है कि उसमें बढ़ोतरी भी दिखे। लेकिन दिक्कत यह रहेगी कि बहुत से छोटे-छोटे कारोबार तबाह होंगे और जो लोग पहले से खरबपति हैं उनका कारोबार बढ़ेगा। अब हिंदुस्तान में सरकारों का जो नजरिया रहने वाला है, उसके मुताबिक छोटे लोगों की नौकरियां जाने और छोटे लोगों के कारोबार खत्म होने से दिल्ली की नींद खराब नहीं होती, और दिल्ली के चेहरे पर शिकन भी नहीं पड़ती क्योंकि जीएसटी के आंकड़े चाहे कहीं से आकर बनते हैं, केंद्र सरकार को ऐसे तमाम आंकड़ों को एक साथ देखने की जरूरत ही होती है। लोगों को याद होगा कि चुनाव से गुजरते हुए दौर में भी उत्तर प्रदेश में एक छोटे कारोबारी ने जो कि भाजपा समर्थक था और भाजपा नेताओं के लिए होर्डिंग लगवाते जिसकी तस्वीरें भी छपी थीं, उसने केंद्र सरकार की टैक्स नीति से थककर, भारी नुकसान झेलकर, फेसबुक लाइव के दौरान बीवी सहित आत्महत्या कर ली थी. उसके पहले उसने सरकार की नीतियों से उसे होने वाली तकलीफ के बारे में बयान भी दिया था।
हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के छोटे कारोबारी ऐसा कुछ करने के बजाय दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे कि वे जिंदा कैसे रह सकते हैं। लेकिन क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार भी हो सकती है जो यह देखें कि मोहल्ला स्तर के जो छोटे-छोटे से कारोबार हैं उन पर कब्जा करने के लिए हमलावर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियों को इससे अलग रखा जाए? ऐसा दिखता तो नहीं है क्योंकि यह सरकार निजी कारोबारियों की हिमायती तो है ही, विदेशी पूंजी निवेश के लिए भी लाल कालीन बिछा कर बाहें फैलाए हुए खड़ी है, और स्वदेशी तो मानो एक अवांछित सा शब्द हो गया है क्योंकि अब तो हथियार बनाने के लिए भी विदेशी पूंजी निवेश का स्वागत है। हो सकता है कि दुनिया के तौर-तरीके अब ऐसे हो गए हैं कि कोई भी देश बहुत लंबे समय तक छोटे कारोबारियों को बचा न सके, लेकिन यह नौबत देश के करोड़ों लोगों के लिए बहुत खतरनाक है और कोई हैरानी की बात नहीं है कि बहुत से छोटे किराना व्यापारी ऐसी बड़ी कंपनियों के सामान पहुंचाने की नौकरी करने को मजबूर हो जाएं, उनका जीना मुश्किल हो जाए। व्यापार को इस बारे में चर्चा करनी चाहिए और खासकर व्यापारियों के जो संगठन हैं, उनको दुनिया की बड़ी कंपनियों से जो खतरा है उस पर बात करनी चाहिए।
यूक्रेन में फंसे हुए हिंदुस्तानी छात्र-छात्राओं को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कई विमान भेजे हैं, और उनमें भारतीय वायुसेना के विमान भी शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 4 मंत्रियों को तैनात किया है जो कि इन्हें वापस लाने के लिए यूक्रेन के अगल-बगल के देशों तक जाकर वहां से उन्हें विमान में चला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के वीडियो कल से तैर रहे हैं जिनमें वे छात्र-छात्राओं को मदद करते दिख रहे हैं, और एक जख्मी छात्रा को सहारा देकर विमान पर चढ़ा रहे हैं। भारत सरकार ने यह घोषणा भी की है कि इन सभी को सरकार अपने खर्च पर वापिस लेकर आएगी। यह एक अच्छी बात है कि सरकार अपने देश के नागरिकों की मदद करने के लिए दुनिया भर में जाकर अपने, या किराए के, और वायु सेना तक के, विमान भेजकर, मंत्रियों को भेजकर, इन छात्र-छात्राओं को मुफ्त में हिफाजत से घर लेकर आ रही है। यूक्रेन जाकर अप्लाई करने वाले हिंदुस्तानी छात्र-छात्राओं में अधिकतर ऐसे हैं जिन्हें हिंदुस्तान के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला नहीं मिल पाया, और यहां के निजी मेडिकल कॉलेजों की करोड़ों रुपए तक जाने वाली फीस देने की उनकी ताकत नहीं थी, इसलिए वे कम फीस वाले यूक्रेन जाकर वहां डॉक्टर बन रहे हैं। यूक्रेन में कुछ साल रहकर डॉक्टर बनने का कुल खर्च शायद 25-50 लाख के भीतर ही होता है, जो कि हिंदुस्तान के मुकाबले खासा कम है, लेकिन है तो सही। इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे परिवारों के थे जो कि महंगी हवाई टिकट भी खरीदने को तैयार थे लेकिन फिर यूक्रेन से विमान उडऩे बंद ही हो गये। पढऩे के लिए दूसरे देश जाने वाले या खासी रकम खर्च करने वाले छात्र-छात्राओं का भी महफूज रहने का अपना अधिकार है, और भारत सरकार की यह जिम्मेदारी भी है। इसलिए आज खबरें सरकार की कोशिशों से भरी हुई हैं। अब जब हर दिन सरकारी विमान यूक्रेन के आसपास के देशों से भारतीय छात्र-छात्राओं को लेकर वापस लौट रहे हैं तो इन खबरों की अहमियत खत्म हो गई है कि समय रहते हुए भारत सरकार ने वहां से भारतीयों को निकलने की न तो चेतावनी दी थी, और न ही कोई इंतजाम किया था।
केंद्र सरकार की यह कोशिशें देखकर याद पड़ता है कि करीब 2 बरस पहले जब हिंदुस्तान में लॉकडाउन हुआ, और एकाएक रेलगाडिय़ां, बस, सबको बंद कर दिया गया, तब किस तरह मजदूर तकलीफें झेलकर महानगरों से और दूसरे प्रदेशों से हिंदुस्तान तक लौटे, अपने गांव वाले हिंदुस्तान तक लौटे। जैसा कि पिछले कुछ समय से लोग लिख भी रहे हैं कि हिंदुस्तान के भीतर भी दो तरह के हिंदुस्तान हैं, तो एक हिंदुस्तान में रहने वाले गरीब लोग उस दूसरे हिंदुस्तान में काम करने गए थे जहां उन्हें काम हासिल था, लेकिन लॉकडाउन के दौर में बिना काम के उन्हें वहां रहने का कोई सहारा नहीं था, महामारी का डर था, और आम लोगों से लेकर केंद्र और राज्य सरकारों तक हर किस्म की अनिश्चितता फैली हुई थी, तो वैसे में लोग अपने बच्चों को गोद में लिए हुए पैदल और साइकिल पर हजार-हजार मील के सफर पर निकल गए थे. उनकी दर्दनाक तस्वीरें इतनी दर्दनाक हैं कि अभी जब फेसबुक पर बहुत से लोगों ने इन्हें पोस्ट करने की कोशिश की तो फेसबुक ने उन्हें एक-एक महीने के लिए ब्लॉक भी कर दिया। जाहिर है कि इन तस्वीरों के खिलाफ फेसबुक पर शिकायतों का सैलाब पहुंचा होगा और उसने इन तस्वीरों को फेक, नकली, दर्ज कर लिया होगा। खैर वह एक अलग बात है मुद्दा यह है कि हिंदुस्तान के ताजा इतिहास में वे दर्दनाक तस्वीरें और वीडियो बहुत अच्छी तरह दर्ज हैं जब इस देश के करोड़ों गरीब मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था, उनके पास न सिर छुपाने को जगह बची थी, और न अगले वक्त के खाने के लिए पैसे थे, और तो और खाना खरीदने की जगह भी बंद थीं।
अगर लोगों की याददाश्त थोड़ा भी साथ देती होगी तो यह भी दो बरस पहले की ही बात है जब केंद्र सरकार ने फैसला लेकर यह घोषणा की थी कि राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों के मजदूरों को अपने खर्च पर वापस लेकर जाएं। हर राज्य ने अपने अफसरों की तैनाती भी की थी और रेलगाडिय़ों के लिए भारत सरकार को एडवांस में भुगतान करके अपने राज्य के मजदूरों को वापस लाने का काम किया था। दो बरस के भीतर की इन दो घटनाओं को देखें तो यह साफ दिखता है कि जो लोग बिना रिजर्वेशन वाले रेल डिब्बे में ही सफर करने की ताकत रखते हैं, उन्हें सब कुछ अपनी जेब से करना है, या फिर वे अपने राज्य की सरकार के रहमो-करम पर छोड़ दिए जाएंगे। दूसरी तरफ 25-50 लाख रुपए खर्च करके जो लोग अपने बच्चों को यूक्रेन या ऐसे किसी दूसरे देश पढऩे के लिए भेज सकते हैं, उन्हें वापस लाना भारत सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, और उन्हें सरकार अपने पैसों पर वापिस लेकर आएगी, उसके मंत्री जाकर इन छात्र-छात्राओं को सहारा देकर विमान में चढ़ाएंगे, और भारतीय वायुसेना के विमान भी इस काम के लिए जाएंगे।
लोगों को अच्छी तरह याद होगा कि चाहे-अनचाहे हिंदुस्तानी मीडिया का कुछ हिस्सा उस वक्त लगातार लॉकडाउन के वक्त की घर वापिसी की खबरों को दिखा रहा था, और उन खबरों को लेकर सबके दिल जले हुए थे, लेकिन उस वक्त की केंद्र सरकार की ऐसी कोई अपील याद नहीं पड़ती कि रास्ते की सरकारें लोगों की मदद करें, केंद्र सरकार की रेलगाडिय़ां मुफ्त में लोगों को उनके गांव के पास के स्टेशन तक पहुंचाएं, केंद्र सरकार की तरफ से लोगों को खाना भी मिल जाए, और खुले में हजार मील चलने वाले बच्चों को दूध मिल जाए। ऐसी कोई भी कोशिश सरकार के तरफ से की गई हो ऐसा याद नहीं पड़ता, और ऐसा दर्ज नहीं है। बिहार में तो डबल इंजिन की सरकार ने तो राज्य की सरहद पर पहुंचे अपने मजदूरों पर लाठियां भी बरसाई थीं. पता नहीं तथाकथित हिंदुस्तानी जनचेतना को यह याद है या नहीं कि किस तरह मध्य प्रदेश लौटते मजदूर थके हुए महाराष्ट्र में पटरियों पर सो गए थे और ट्रेन तले थोक में कट गए थे।
आज यूक्रेन से अपने बच्चों को वापस लाने के लिए सरकार की कोशिश खबरों में तारीफ पा रही है, लेकिन हिंदुस्तानी याददाश्त इतनी कमजोर है कि वह मजदूरों की घर वापसी को पूरी तरह भूल चुकी है और वैसे भी उन मजदूरों के साथ हिंदुस्तान की जनता के एक हिस्से की हमदर्दी कभी भी नहीं रहती जिन्हें मजदूरी के लिए दूर-दूर दूसरे प्रदेश तक जाना पड़ता है। इतने कमजोर लोगों के साथ तो उस तथाकथित ईश्वर की भी हमदर्दी नहीं रहती जो सर्वशक्तिमान है, और जिसने इन मजदूरों की ऐसी हालत देखी हुई है, तय की हुई है। एक लोकतंत्र का इतिहास कई किस्मों की मिसालों की तुलना दर्ज करता है। आज यह छोटी सी बात हमारे दिमाग में आ रही है, और आगे जाकर जब कभी हिंदुस्तानी लोकतंत्र का इतिहास लिखा जाएगा तो इस देश के ताजा, नवोदित इतिहासकारों से परे, इस देश के बाहर के कुछ ऐसे इतिहासकार भी होंगे, जिन्हें यूक्रेन से घर वापिसी और मुंबई दिल्ली से घर वापिसी में सरकार के रुख और नजरिये का फर्क दिखेगा। लोकतंत्र में तंत्र तो अपनी मनमर्जी कर सकता है, लेकिन लोक को तो तमाम बातों को जोडऩा, और उन पर सोचना चाहिए। उसके बिना उनका तंत्र में पिस जाना तय रहता है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
हिन्दी के एक टीवी अभिनेता ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील लगाई है कि उनसे जिंदगी में हुई एक गलती का जिक्र इंटरनेट से हटाया जाए। बहुत बरस पहले जब यह अभिनेता एक नौजवान था, उसने एक बार शराब पीकर गाड़ी चलाई थी और उसका केस बना था। तबसे अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है, लेकिन शराबी ड्राइविंग का यह मामला इंटरनेट पर बना हुआ है, और इस अभिनेता का नाम सर्च करने पर तुरंत सामने आ जाता है। अब क्या लोगों की पुरानी जिंदगी की बातों को उसी तरह मिटाया जा सकता है जिस तरह हिन्दुस्तान के इतिहास की जानकारियों को इन दिनों मिटाया जा रहा है? या फिर उन्हें मिटाने का किसी को हक नहीं हो सकता। जैसा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट को लेकर बाकी मामलों में है, हिन्दुस्तान पश्चिम के विकसित और सभ्य लोकतंत्रों से खासा पीछे चलता है, और इसलिए अभी हिन्दुस्तान में न किसी को शादीशुदा जिंदगी में बलात्कार की परवाह है, और न ही इंटरनेट से अपना इतिहास हटवाने के मुद्दे पर गौर करने की।
लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या एक कानूनी सजा या जुर्माना ही किसी की गलती या गलत काम के लिए काफी रहते हैं, या फिर उन्हें लेकर समाज और सोशल मीडिया में होने वाली बदनामी भी जरूरी होती है? अब जैसे किसी परिवार के किसी व्यक्ति ने घर के बाहर कहीं बलात्कार कर दिया, तो उसके परिवार की इसमें सहमति तो नहीं रहती है, लेकिन बदनामी तो पूरे परिवार की होती है, पिछली पीढ़ी की अगली पीढ़ी की या साथ-साथ जीवन साथी की भी। कुछ मामलों में किसी जाति या धर्म के लोग कोई जुर्म करते हैं, और पूरे समुदाय की बदनामी होती है, पूरे समुदाय को अविश्वास से देखा जाता है। इसलिए सजा सिर्फ कानून की सुनाई हुई नहीं होती, सिर्फ मुजरिम को नहीं मिलती, और सिर्फ वक्ती तौर पर नहीं रहती, बल्कि वह साये की तरह जिंदगी भर साथ-साथ भी चलती है।
पुराने वक्त से चली आ रही सामान्य समझबूझ भी यह कहती है कि साख राख, और खाक तक साथ जाती है, यानी इंसान का बदन राख हो जाता है, या खाक में मिल जाता है, फिर भी साख बनी रहती है। इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट में दायर इस अपील से परे भी आम सोच यही कहती है कि जिंदगी भर बदनामी या तोहमत को झेलना सजा का एक हिस्सा होता है। लोगों को कुछ भी करने के पहले आगे की अपनी लंबी जिंदगी की साख या बदनामी भी सोचनी चाहिए, अपने आसपास के लोगों की इज्जत के बारे में भी सोचना चाहिए जो कि बेकसूर रहते हुए भी बदनामी की सजा भुगतते हैं। कई मामलों में तो यह हो जाता है कि बलात्कारियों की आल-औलाद की शादियां भी आसानी से नहीं हो पातीं, या कई किस्म के समझौते करके ही हो पाती हैं। दुनिया के इतिहास में लोगों को बड़े बन जाने पर अपने बचपन की भी छोटी-छोटी गलतियों की साख ढोनी पड़ती है क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचने वाले लोगों की नींव को इतनी गहराई तक खोदा जाता है कि उनके बचपन की गलतियां तक उजागर हो जाती हैं। हमने पहले भी इस जगह यह लिखा है कि सोशल मीडिया पर हिंसा और अश्लीलता लिखने वाले लोगों को याद रखना चाहिए कि आगे जब कभी वे किसी नौकरी के लिए अर्जी देंगे, या किसी बड़े विश्वविद्यालय में दाखिला चाहेंगे तो उनका सोशल मीडिया खंगाला जा सकता है, और यह देखा जा सकता है कि वे लोगों को किस तरह की धमकियां देते आए हैं।
वैसे आज की विकसित और कारोबारी दुनिया में बहुत सी ऐसी डिजिटल एजेंसियां काम कर रही हैं जो भुगतान करने की ताकत रखने वाले लोगों के सार्वजनिक-डिजिटल इतिहास की अप्रिय और अनचाही बातों को हटवाने का काम करती हैं। मतलब यह कि अगर आपकी ताकत है तो आप अपनी बदनामी भी कुछ या काफी हद तक मिटवा सकते हैं। लेकिन यह सहूलियत हर किसी को हासिल नहीं रहती, और जो लोग आज सोशल मीडिया पर किसी धर्म, जाति, या राजनीतिक विचारधारा के तहत, या ऐसे तबकों से मिलने वाले किसी भुगतान के एवज में अगर सोशल मीडिया पर जुर्म करते चल रहे हैं, तो उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उनका यह जुर्म रिकॉर्ड से हट नहीं सकता। लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की पेशेवर और माहिर खुफिया एजेंसियां इंटरनेट की शुरूआत से अभी तक का इतिहास खंगाल कर कई लोगों के बारे में यह जानकारी भी निकालकर रखती है कि जब 25 बरस पहले इंटरनेट पर बच्चों से सेक्स के चैटरूम हुआ करते थे, उस वक्त की चैट भी आज खुफिया एजेंसियों के पास है, और इसका इस्तेमाल बहुत से लोगों को धमकाने या ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। इसलिए कुल मिलाकर रास्ता यही है कि राह से भटकने से ही बचा जाए, वरना अगर आप आम हैं, तो आम बदनामी के शिकार रहेंगे, और अगर खास हैं, तो खास जासूसों की खास निगरानी का शिकार रहेंगे। आज की दुनिया में इंटरनेट और सोशल मीडिया से किसी के बारे में सब कुछ मिटा पाना नामुमकिन है। इसलिए शराफत में ही समझदारी है...
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
पश्चि एशिया के एक अरब देश जॉर्डन की एक महिला, हदील दवास अपने बच्चों को जंगल, पहाड़, और नदी किनारे घुमाने ले जाती हैं। एक बच्चे को पीठ पर, और दूसरे का हाथ थामकर, और खाने की बॉस्केट लिए हुए वे अक्सर कुदरती खूबसूरती की जगहों पर अपने बच्चों को ले जाती हैं, और फिर जाने लायक ऐसी जगहों के बारे में, वहां के रास्ते के बारे में वे अपने इंस्टाग्राम अकाऊंट पर लोगों को जानकारी भी देती हैं कि बच्चे कहां ले जाए जा सकते हैं, कहां वे खुद चल सकते हैं। दस बरस से वे अपना यह शौक पूरा कर रही हैं, और बहुत से दूसरे लोगों को उनसे एक रास्ता भी दिख रहा है। उनका यह कहना है कि कुदरत के पास जाकर बच्चे बहुत खुश होते हैं, खूब खेलते हैं। हदील पेशे से आर्किटेक्ट हैं, और उन्होंने अमरीका से मास्टर्स डिग्री भी ली हुई है, और वे ट्रैवल फॉर पीस नाम की एक संस्था चलाती हैं जो कि ऐसे कुदरती पर्यटन को बढ़ावा देती है।
आज हिन्दुस्तान में अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो बहुत से लोग तो जिंदगी की मजबूरियों के बोझ से इस तरह लदे हुए रहते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए अधिक कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे तबके भी मौजूद हैं जो ठीकठाक कमा लेते हैं, जो बच्चों पर कुछ वक्त और कुछ पैसा खर्च भी करते हैं, लेकिन उनके बीच भी बच्चों को प्रकृति को दिखाने ले जाना, प्रकृति के साथ उन्हें वक्त गुजारने देना कम ही सुनाई पड़ता है। कुछ हद तक लोग साल-छह महीने में एक बार कहीं पर्यटन पर जाने पर बच्चों को नदी-पहाड़ या समंदर दिखा देते हैं, या फिर कुछ मामलों में पिकनिक पर जाने पर बच्चों को जंगल या नदी के किनारे देखने मिल जाते हैं। लेकिन सिर्फ कुदरत के करीब ले जाने के हिसाब से शायद ही कोई अपने बच्चों को ले जाते हैं। शहरों में तो लोगों की पहली प्राथमिकता अपने बच्चों को कारोबारी मॉल ले जाने की रहती है, जहां वे फिल्में देखें, खरीददारी करें, बड़े ब्रॉंड का कुछ खाना खाएं, या फिर वहां के किसी प्ले जोन में महंगे खेल खेल लें। हर बच्चे पर सैकड़ों या हजारों रूपए खर्च करके आधा दिन गुजारकर लोग इस तसल्ली से लौट आते हैं कि आज उन्होंने बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजार लिया। दरअसल बाजार की सारी साजिश यही रहती है कि लोगों को ऐसी संतुष्टि मिले कि बच्चों पर खर्च उनकी बेहतर देखरेख है। बच्चों के लिए महंगे सामान खरीदना लोगों को उनकी फिक्र करना लगता है। ऐसे में जॉर्डन की इस महिला की चर्चा करना हमें जरूरी लग रहा है कि जिन लोगों के पास साधन और सुविधाएं हैं, कम से कम वे लोग तो अपने बच्चों को कुदरत से रूबरू करवाते चलें, और यह बात महज एक नमूने के लिए नहीं है बल्कि जब समय रहे बार-बार करने के लिए है ताकि बच्चों को प्रकृति का महत्व समझ आए, और उसके साथ जीना सीख सकें।
आज घरों में छोटे-छोटे बच्चे भी टीवी पर कॉर्टून फिल्मों, या मोबाइल पर किसी वीडियो गेम के ऐसे आदी हो चुके हैं कि वे दूध पीने या खाना खाने के लिए भी इन चीजों की जिद करते हैं, और मां-बाप को मजबूर करते हैं कि वे स्क्रीन शुरू करके उन्हें दें। ऐसे में कमउम्र से ही बच्चों को स्क्रीन और शहरी-आधुनिक उपकरणों के बिना भी जीना सिखाना चाहिए, और यह काम अधिक मुश्किल भी नहीं है अगर मां-बाप खुद फोन और कम्प्यूटर छोडक़र बच्चों को लेकर बाहर निकलें, और स्क्रीन से परे की जिंदगी उन्हें दिखाएं। नदी और पहाड़ तक ले जाना, समंदर या जंगल तक ले जाना, और वहां पर पशु-पक्षियों की आवाजें सुनने देना, ऊंचे पेड़ों से लेकर पतझड़ के बिखरे पत्तों तक से उन्हें रूबरू करना, सुरक्षित-उथली नदी के किनारे उनके पांव पानी में उतारकर उन्हें यह प्राकृतिक पानी महसूस करने देना जैसी कई बातें हो सकती हैं जो इन बच्चों को पहली बार देखने, सुनने, और छूने मिलें, और हर बार उन्हें इनका अलग-अलग तजुर्बा हो। हो सकता है कि वे वहां से कोई चिकना पत्थर लेकर लौटें, और घर पर उस पर चित्रकारी करते हुए कुछ वक्त गुजारें। ऐसी बहुत सी बातें बच्चों को कुदरत के करीब ले जाने से उनकी कल्पना और सोच को विकसित करने में मदद कर सकती हैं, शर्तिया करेंगी, और वे एक बेहतर इंसान बनेंगे। लेकिन आज अधिकतर मां-बाप अपनी अधिकतम सहूलियत के मुताबिक बच्चों को शहर के किसी मॉल या किसी प्ले जोन ले जाकर, आइस्क्रीम पॉर्लर या किसी फास्टफूड सेंटर ले जाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं, जिनसे बच्चों का कोई भी विकास नहीं हो पाता।
इंस्टाग्राम पर जॉर्डन की इस हिजाबधारी मुस्लिम महिला ने अपने बच्चों की ऐसी प्राकृतिक सैर की जो तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करना शुरू किया है तो उसने दसियों हजार लोगों को प्रेरणा दी है, और लोग अपने बच्चों को वक्त गुजारने और मनोरंजन का एक बेहतर विकल्प दे पा रहे हैं। साल में एक या दो बार किसी दूसरे प्रदेश या देश जाना एक अलग बात है, लेकिन हर हफ्ते-पन्द्रह दिन में आसपास के किसी नदी-पहाड़, जंगल-झरने तक बच्चों को ले जाना उनकी जिंदगी का रूख बदल सकता है, और अब तो ऐसे सैर-सपाटे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोग दूसरे लोगों के बीच भी इस सकारात्मक पहल को बढ़ावा दे सकते हैं। हो सकता है कि लोग अपने दोस्तों के बीच इस किस्म के समूह बनाएं जिनमें वे आसपास की ऐसी जगहों की चर्चा करें, और यह भी हो सकता है कि कुछ परिवार मिलकर भी बच्चों को ऐसी जगहों पर ले जाएं। यह इतनी सामान्य समझ की बातें हैं कि इस बारे में हमें अधिक खुलासे से यहां लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को मॉल से बाहर निकालने के लिए इस मुद्दे पर चर्चा की जरूरत जरूर लगी थी, इसलिए आज जॉर्डन की इस महिला की मिसाल देकर यह बात छेड़ी गई।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
हिन्दुस्तान के एक सोलह बरस के शतरंज खिलाड़ी, ग्रैंडमास्टर आर प्रागननंदा ने अभी लोगों को हैरान कर दिया जब उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाईन शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। माथे पर सफेद तिलक लगाए हुए प्रागननंदा की तस्वीरें पूरी दुनिया में फैल रही हैं, और लोग इस जीत पर हैरान हैं। लेकिन इतनी कमउम्र में दुनिया के एक सबसे माहिर शतरंज खिलाड़ी को हराने की इस खबर की दो छोटी-छोटी और बातें बड़ी दिलचस्प हैं। पहले से तय इस ऑनलाईन शतरंज टूर्नामेंट के ठीक पहले प्रागननंदा ने दिमागी आराम के लिए भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 मैच देखा था। और फिर इस शतरंज मुकाबले में दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी को हराकर वह चैन से सोने चला गया था, बिना कोई जश्न मनाए।
अब यह सोचने की बात है कि शतरंज मुकाबले के ठीक पहले यह किशोर खिलाड़ी क्रिकेट मैच देख रहा था। हिन्दुस्तान में आमतौर पर औसत छात्र-छात्राएं इम्तिहान के मिनट भर पहले तक कॉपी-किताब में डूबे रहते हैं, पिछली रात जागकर पढ़ते रहते हैं, और दिमाग को आराम जरा भी नहीं देते। किसी काम में कामयाब होने के लिए मेहनत के साथ-साथ आराम की भी जरूरत होती है, इसके महत्व को वे लोग नहीं समझ पाते जो लोग मेहनत को ही सब कुछ मानकर चलते हैं। मेहनत का अपना एक महत्व होता है, लेकिन मेहनत के बीच आराम का भी एक महत्व होता है। जो लोग कसरत करते हैं उन्हें यह बात मालूम रहती है कि हफ्ते में एक या दो दिन का आराम भी जरूरी रहता है। अधिक गंभीरता से कसरत करने वाले महीने में तीसों दिन कसरत नहीं करते क्योंकि बदन को आराम की जरूरत होती है तभी वह आगे काम के लायक तैयार हो पाता है। ठीक इसी तरह शतरंज जैसा दिमागी काम करने वाले लोगों को भी इस खेल से परे के आराम या मनोरंजन की जरूरत होती है, और इसीलिए कोई क्रिकेट टीम चाहे आलोचना का शिकार होती रहे, वह किसी बड़े मैच के पहले कभी स्वीमिंग पूल में खेलते दिखती है, तो कभी किसी और तरह का मनोरंजन करते।
लोगों को जिंदगी में विविधता का भी सम्मान करना चाहिए, और अपने खास मकसद में लगे हुए भी उन्हें अपने तन-मन को आराम देने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि लगातार मेहनत से जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई भी बीच-बीच में होते रहनी चाहिए। शायद यही वजह थी जो यह किशोर शतरंज खिलाड़ी शतरंज की बिसात पर और मेहनत करने के बजाय क्रिकेट मैच देखकर अपने को तरोताजा कर रहा था। पढ़ाई के किसी इम्तिहान या किसी दाखिला-इम्तिहान की तैयारी में रात-दिन लगे हुए बच्चों के मां-बाप को भी यह समझना चाहिए कि इन बच्चों को बीच-बीच एक ब्रेक की जरूरत होती है तभी वे आगे की मेहनत करने के लायक तैयार हो सकते हैं। आम हिन्दुस्तानी मां-बाप की दिक्कत यह है कि वे न सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई तय करते हैं, उनका रोजगार तय करते हैं, बल्कि वे उनका मनोरंजन भी तय करने पर आमादा रहते हैं कि उन्हें किस तरह का मनोरंजन करना चाहिए। इससे बच्चों की मौलिकता पूरी तरह खत्म हो जाती है, और आज अगर कोई हिन्दुस्तानी लडक़ा दुनिया के सबसे बड़े शतरंज खिलाड़ी को हरा रहा है, तो यह महज किसी तकनीक को सीखकर नहीं कर पाया है, बल्कि अपनी कुछ मौलिक चालों की वजह से वह उस्ताद को शिकस्त दे पाया है। इसलिए लोगों को खुद भी अपनी मौलिकता का सम्मान करना चाहिए, और अपने आसपास के लोगों की मौलिकता को भी बनाए रखना चाहिए। संगीत के छात्र शास्त्रीय संगीत की बारीकियों की तकनीक को सीख सकते हैं, बने बनाए राग को सीख सकते हैं, लेकिन एक अनोखा संगीत बनाने के लिए उन्हें अपने मौलिक संगीत पर ध्यान देना होता है, तभी जाकर कोई संगीत उल्लेखनीय बन पाता है और चर्चा पाता है।
प्रागननंदा की इस जीत की खबर में यह भी देखने की जरूरत है कि किस तरह वह जिंदगी की सबसे बड़ी जीत को पाकर बिना इसकी खुशी मनाए सोने चले गया। लोगों में अपनी कामयाबी पर भी अपने दिमाग को काबू में रखना आना चाहिए। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी अगर कोई चैन से सो सकता है, तो ऐसा लगता है कि वह उससे भी बड़ी कामयाबी के लायक है। कुछ लोगों को लग सकता है कि हम बड़ी मामूली और छोटी-छोटी बातों के बड़े-बड़े मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को अपनी जिंदगी में ऐसी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान भी देना चाहिए, और अपने आसपास के लोगों को भी उनके मनचाहे तरीकों से मनोरंजन करने या आराम करने की रियायत देनी चाहिए जो कि लोग देना नहीं चाहते हैं।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
हिन्दुस्तान में जिस हिन्दी भाषा को हम समझते हैं उसमें बच्चों के साहित्य का मामला हमेशा से कुछ गड़बड़ रहा है। एक तो बच्चों के लिए अच्छा साहित्य लिखने वाले लोग कम रहते हैं, और जो रहते हैं उनकी अपनी राजनीतिक समझ और सामाजिक सरोकार दोनों ही कमजोर रहते हैं। नतीजा यह होता है कि वे कमल को घर चलने कहते हैं, और कमला को जल भरने कहते हैं। पहला लैंगिक भेदभाव बचपन की सबसे कच्ची उम्र में ही शुरू होता है जहां स्कूली किताबों से लेकर कहानियों तक मां और बहन को घर का काम करने वाला बताया जाता है, और पिता बाहर काम करने वाले, और बेटा राजा भैया रहता है। लेकिन लैंगिक भेदभाव से परे भी हिन्दुस्तान बाल साहित्य की संवेदनाएं बड़ी कमजोर हैं, और उनसे मिलने वाली चेतना बच्चों को एक कमजोर नागरिक ही बना पाती है। दरअसल बहुत से लोग इस मामले को बच्चों के विकास से जोडक़र देखते भी नहीं हैं, और अधिकतर लोगों को यह समझ ही नहीं आता कि बाल साहित्य से बच्चों के विकास का कुछ खास लेना-देना होता है।
संपन्न तबका तो अपने बच्चों को अंग्रेजी की कार्टून फिल्मों से लेकर अंग्रेजी के बाल साहित्य तक और अंग्रेजी स्कूली किताबों तक को देकर छुट्टी पा लेता है, जो कि लैंगिक समानता के पैमाने पर हिन्दी के मुकाबले कुछ बेहतर रहती हैं। लेकिन हिन्दी का मामला तो बहुत ही गड़बड़ है। और लैंगिक समानता से परे भी बाल साहित्य के साथ दिक्कत यह है कि उसे सतही तुकबंदी से बनाया गया सामान मान लिया जाता है। हिन्दी में नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा वो काले चोर ले गए, सबको बहुत पसंद आने वाला गाना है। लेकिन इस गाने पर हावी रंगभेद को अगर देखें तो यह समझ पड़ता है कि यह गाना हिन्दी में ही लिखा जा सकता था, और दक्षिण भारत में यह मुमकिन नहीं था। चोर काला होता है, यह बताते हुए बच्चों के दिमाग में यह भी बिठा दिया जाता है कि काले लोग चोर होते हैं, या हो सकते हैं। ऐसी बात उत्तर भारत के अपेक्षाकृत कम काले या गोरे हिन्दीभाषी ही लिख सकते थे। अभी एकलव्य नाम की एक प्रतिष्ठित संस्था की प्रकाशित बच्चों की एक किताब देखने मिली जिसमें एक कविता है, मोटी अम्मा, मोटी अम्मा पिलपिली, बच्चा लेकर गिर पड़ी, बच्चे ने मारी लात, चल पड़ी बारात, बारात के नीचे अंडा, खेलें गिल्ली-डंडा। अब मासूम से दिखने वाले इन शब्दों को अगर देखें तो उनके पीछे भारी बदन वाली किसी महिला की उसके बदन के आकार के लिए सीधे-सीधे खिल्ली उड़ाना सिखाया गया है। मोटी महिला गिर रही है, और बच्चा लात मार रहा है, और कवि इसे पिलपिली महिला कह रहा है! आज सोशल मीडिया पर अंग्रेजी भाषा में जिसे बॉडी-शेमिंग कहा जाता है, शरीर के आकार को लेकर धिक्कारना या खिल्ली उड़ाना, वह कविता के इन गिने-चुने शब्दों में भरा हुआ है। एकलव्य की इसी किताब में बॉडी शेमिंग की एक दूसरी मिसाल भी है, एक प्लेट में दो आलू, मोटू बोला मैं खा लूं, खाते-खाते थक गया, रोटी लेकर भग गया, रोटी गिर गई रेत में, मोटू रोया खेत में। जाहिर है कि इस किताब को तैयार करने वाले लोगों को मोटापे की खिल्ली उड़ाने से कोई परहेज नहीं है, और इसे पढऩे वाले बच्चे अपनी क्लास के किसी मोटे बच्चे की खिल्ली अगर उड़ाएंगे, तो वे अपनी नजरों में कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे। इसी किताब की एक और कविता कहती है, टेसू बेटा बड़े अलाल, खाते बासी-रोटी-दाल, बासी दाल ने किया धमाल, टेसू की मुंडी से उड़े बाल, चिकनी मुंडी चाय गरम, टेसू राजा बेशरम। अब दस-बीस शब्दों की इस कविता में बासी खाने वालों को अलाल भी बता दिया गया, बासी खाने से सिर के बाल उडऩा भी बता दिया गया, सिर के बाल उडऩे वाले को चिकनी मुंडी वाला बेशरम भी बता दिया गया! यह सिलसिला बहुत ही खतरनाक है।
हिन्दी की पाठ्य पुस्तकों में बच्चों के लिए बनाई गई कहानियों और कविताओं में से बहुतों का यह हाल रहता है। और यह सिलसिला बदलने की जरूरत है। भाषा को न्यायसंगत और सामाजिक सरोकार का बनाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बच्चों की सोच की बुनियाद से ही अगर उनके मन में सामाजिक भेदभाव या शरीर को लेकर हिकारत भर दी जाए, तो वे जिंदगी भर वैसे ही पूर्वाग्रहों के साथ जीने का खतरा रखते हैं। आज जब हिन्दुस्तान में एक संकीर्णतावादी सोच छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक की पढ़ाई को एक खास धर्म और तथाकथित संस्कृति के मुताबिक ढालने पर आमादा है, उस वक्त ऐसी महीन बातों पर सोचने की किसी को फुर्सत भी नहीं है, और सरकारी किताबों से परे निजी किताबों के लेखकों-प्रकाशकों में भी सामाजिक-चेतना की भारी कमी है। ऐसे में जिम्मा समाज के जागरूक तबकों का बनता है कि वे जहां कहीं गैरबराबरी और बेइंसाफी की बातों को लिखा देखें, उनका विरोध करें।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
अभी भारत के क्रिकेट सितारे सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि की कही हुई कुछ बातें एक खबर में छपी हैं कि किस तरह उन्होंने परिवार का ख्याल रखने के लिए अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ी ताकि सचिन तेंदुलकर पूरी तरह से क्रिकेट में ध्यान लगा सकें। यह कतरन कुछ लोगों ने फेसबुक पर पोस्ट की तो लोगों ने अंजलि के त्याग की बड़ी तारीफ की, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि त्याग हर बार महिला को ही क्यों करना होता है? खासकर हिन्दुस्तान में यह बात और तल्खी के साथ नजर आती है कि लोग आमतौर पर पढ़ी-लिखी बहू चाहते हैं, और साथ ही यह भी चाहते हैं कि वह अगर बाहर काम करती है तो भी उसके साथ-साथ घर को भी अच्छी तरह सम्हाले, और अगली-पिछली सभी पीढिय़ों का भी ठीक से ख्याल रखे। यह गैरबराबरी अगर हिन्दुस्तान जैसे देश में ही रहती तो भी समझ में आता, लेकिन यह सबसे विकसित और लोकतांत्रिक देशों में भी जिस हद तक सामने आती है वह बात चौंकाने वाली है।
अभी दो दिन पहले ही जर्मनी की कामकाजी महिलाओं के बारे में एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि योरप के एक सबसे सभ्य और विकसित लोकतंत्र में भी बराबर पढ़ी-लिखी हुई महिलाएं आगे बढऩे की अपनी संभावनाओं के मामले में बराबरी के पुरूषों से किस हद तक पीछे रह जाती हैं। गैरबराबरी का यह फासला घट जरूर रहा है, लेकिन अभी भी यह काफी बड़ा है। पढ़ाई और काबिलीयत के मामले में जर्मन महिलाएं आदमियों से आगे हैं, कामगारों के बीच भी उनका अनुपात बराबरी से थोड़ा ही कम है, लेकिन नौकरियों में सबसे सीनियर ओहदों पर उनकी हिस्सेदारी आदमियों के मुकाबले बहुत कम है। 160 बड़ी जर्मन कंपनियों के बोर्ड स्तर पर कुल 11 फीसदी महिलाएं हैं, और आम जर्मन महिलाओं की तनख्वाह भी पुरूषों के मुकाबले करीब 20 फीसदी कम है। तनख्वाह का फर्क घट रहा है लेकिन औसत रूप से महिलाओं को पुरूषों के मुकाबले रिटायरमेंट पेंशन 49 फीसदी कम मिलती है। लेकिन इसकी पूरी तोहमत लैंगिक भेदभाव पर डालना सही नहीं होगा क्योंकि परिवार का ख्याल रखने या बच्चों को बड़ा करने के लिए महिलाएं अपना करियर ठीक उसी तरह कुर्बान कर रही हैं जिस तरह की बात अंजलि तेंदुलकर के बारे में अभी सामने आई है।
हिन्दुस्तान के बारे में कुछ समय पहले एक आंकड़ा सामने आया था कि 2005 में भारतीय मजदूरों में महिलाओं का अनुपात 26 फीसदी था जो कि 2019 में घटकर 20 फीसदी रह गया है। विश्व बैंक के इन आंकड़ों को इस संदर्भ में देखना बेहतर होगा कि भारत के इस 20 फीसदी के मुकाबले बांग्लादेश में महिला कामगारों की भागीदारी 30.5 फीसदी है, और श्रीलंका में यह संख्या 33.7 फीसदी है। भारत के कामगारों में 30 फीसदी महिलाएं संख्या में जरूर काम कर रही हैं, लेकिन वे सबसे निचली मजदूरी पाने वालों में हैं। हिन्दुस्तानी उद्योग-धंधों की एक तकलीफदेह हकीकत यह भी है कि शादी या बच्चों के लिए कुछ लंबी छुट्टी लेने वाली महिलाओं का काम खो बैठने का खतरा बहुत अधिक होता है। अब सवाल यह है कि शादी के बाद नए घर जाकर रहने, शहर बदलने की समस्या महिला की ही रहती है, हिन्दुस्तान में तो आदमियों की यह दिक्कत नहीं रहती है। और गर्भवती भी महिलाएं ही होती हैं, इसलिए उन्हीं को प्रसूति अवकाश लेना होता है, कानूनन उन्हें ही मिलता है, और बच्चे बड़े करने की जिम्मेदारी भी उन पर होती है, परिवार के बुजुर्गों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर रहती है। इस तरह उनके कामकाज की जगहों पर उन्हें लेकर अनिश्चितता का खतरा अधिक रहता है, और यह अनिश्चितता उनके वेतन-भत्तों से लेकर नौकरी की सुरक्षा की गारंटी तक सभी पर असर डालता है।
तो क्या यह मान लिया जाए कि देश कैसा भी, अर्थव्यवस्था कैसी भी हो, बच्चे पैदा करने और परिवार देखने की जिम्मेदारियां महिलाओं को कभी भी बराबरी का हक और बराबरी की संभावनाएं नहीं पाने देंगी? यह गैरबराबरी तब और अधिक बढ़ जाती है जब कोई समाज या इलाका महिलाओं को सुरक्षित आवाजाही और काम की सुरक्षित जगह नहीं दे पाता। ऐसे में एक महिला का कामकाज के लिए रात-दिन का आना-जाना मुमकिन नहीं हो पाता, और काम की उनकी जगहों पर वे बराबरी की संभावनाएं नहीं छू पातीं। पुरूष कर्मचारियों के साथ यह सहूलियत रहती है कि उनकी दिन-रात कभी भी ड्यूटी लगाई जा सकती है, वे काम पर आ-जा सकते हैं, लेकिन महिलाओं को ऐसा सुरक्षित वातावरण नहीं मिल पाता, और हिन्दुस्तान जैसे देश में तो अधिकतर जगहों पर उन्हें रात में अकेले आने-जाने की हिफाजत भी हासिल नहीं रहती।
इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि घर पर काम करने वाली महिला की उत्पादकता को आर्थिक पैमाने पर नापने की कोई परंपरा नहीं है। घर पर उसके किए हुए रोजाना के दस-बारह घंटे या और अधिक के काम का कोई मूल्यांकन नहीं होता है, और उसे मिलने वाली सिर छुपाने की जगह, दो वक्त का खाना, और सामाजिक सुरक्षा को ही उसकी मजदूरी मान लिया जाता है। जबकि एक महिला के किए जाने वाले अलग-अलग तरह के रोजाना के काम, और परिवार की सुरक्षा में उसकी लगने वाली मेहनत को अगर देखा जाए, तो इन सबको हासिल करने के लिए किसी भी परिवार को बहुत बड़ी रकम खर्च करनी होती, लेकिन ऐसी मेहनत का कोई मूल्यांकन नहीं होता। महिलाओं से जुड़े हुए इन तमाम मुद्दों पर अलग-अलग मंचों पर बार-बार चर्चा करने की जरूरत है क्योंकि महिला के हाथ में उसकी मेहनत का जायज मेहनताना चाहे न आए, कम से कम परिवार और समाज में उसे यह महत्व और सम्मान तो मिलना ही चाहिए कि वह नगदी मेहनताना पाए बिना भी अपनी सहूलियतों से सौ गुना अधिक योगदान परिवार और समाज को देती है। अंजलि तेंदुलकर ने अगर काम छोडक़र परिवार सम्हाला, और सचिन तेंदुलकर को परिवार की तरफ से बेफिक्र रहकर हिन्दुस्तान का सबसे अधिक कमाऊ भारत रत्न बनने मिला, तो इसमें घरवाली के योगदान का मूल्यांकन जरूरी है।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
अभी अनायास एक ऐसा वैज्ञानिक संयोग हुआ जिसने यह अंदाज लगाने का मौका दिया है कि इंसान अपने आखिरी कुछ पलों में क्या करते हो सकते हैं? अमरीका की एक यूनिवर्सिटी, लुईसविले, में न्यूरोसर्जन एक ऐसे व्यक्ति की दिमागी हलचलों को रिकॉर्ड कर रहे थे जो कि मिर्गी के दौरों का शिकार था। उसके दिमाग की तरंगें दर्ज हो ही रही थीं कि वह अचानक दिल के दौरे से मर गया। अब मौत के कुछ पल पहले, और दिल की धडक़न बंद हो जाने के बाद के कुछ पलों तक उसके दिमाग में जो हलचल चल रही थी उसे कम्प्यूटर रिकॉर्ड करते चल रहा था। अब वैज्ञानिकों के पास ऐसी तकनीक है कि वे ऐसी रिकॉर्डिंग का यह विश्लेषण कर सकते हैं कि उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था। इस व्यक्ति के मौत के वक्त की रिकॉर्डिंग बतलाती है कि वह सपने देखते हुए या पुरानी यादों को ताजा करते हुए दर्ज होने वाली रिकॉर्डिंग सरीखी थीं। इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि मौत के वक्त उस इंसान के दिमाग में अपनी जिंदगी की यादों का सैलाब चल रहा था। अब यह बात एक वैज्ञानिक अध्ययन के एक मानवीय विश्लेषण से निकली हुई है, और यह अपने किस्म की एक अनोखी और अकेली रिकॉर्डिंग है इसलिए इससे बहुत अधिक निष्कर्ष निकालना भी जायज नहीं होगा। आज इस जगह पर इस मुद्दे को लेकर लिखने का मतलब ऐसे वैज्ञानिक विश्लेषण की गहराई में जाना नहीं है, बल्कि इसके एक मानवीय पहलू पर चर्चा करना है।
अगर यह बात और कई लोगों की रिकॉर्डिंग में साबित होती है कि मौत के पल इंसान की जिंदगी की यादों को दुहराने के पल रहते हैं, तो फिर लोगों को यह सोचना चाहिए कि वे अपने ऐसे पलों के लिए अपनी जिंदगी में किस किस्म की यादें रखना चाहते हैं? वैसे भी धर्म से जुड़े हुए लोग भी यह कहते हैं कि मौत के बाद ऊपर जाकर तमाम चीजों का हिसाब देना होता है। अगर ऐसा कोई ऊपर है, और वहां ऐसा कोई हिसाब होता है, तो उस हिसाब में भी लोगों को जिंदगी की तमाम अच्छी और बुरी यादों से गुजरना ही होगा। इसलिए आज बेहतर यही है कि वैज्ञानिक निगरानी में दर्ज होने वाले आखिरी पलों की बात हो, या ऊपर जाकर किसी काल्पनिक ईश्वर के सामने हिसाब देने की बात हो, लोगों को अपनी जिंदगी के अंत के लिए अपनी यादों को बेहतर रखना चाहिए। कुछ लोगों को यह भी लग सकता है कि केवल किस्से-कहानियों में चल रही ईश्वर की अदालत की परवाह करके भला क्यों पूरी की पूरी जिंदगी ईमानदारी की तकलीफ में गुजारें, या बेईमानी का मजा पाने से परे रहें। लेकिन कुछ लोग ऐसा जरूर सोच सकते हैं कि आखिरी वक्त अपनी छाती पर इतना बोझ न रहे कि यादें ही अपना गला घोंट दें।
जो बात हम लिख रहे हैं यह बहुत ही महीन बात है, और मोटी समझ वाले, नैतिकता से बेफिक्र अधिकतर लोगों के लिए यह बेवकूफी की एक गैरजरूरी बात होगी। लेकिन फिर भी हमें जो सूझ रहा है वह यह है कि लोगों को अपनी पूरी जिंदगी ऐसे काम भी करने चाहिए जो कि आखिरी वक्त पर अपनी छाती का बोझ हल्का कर पाएं। लोगों को यह भी सोचकर जिंदगी गुजारनी चाहिए कि कुछ अच्छी यादें भी इन आखिरी पलों के लिए साथ रहें, और जिनका भरोसा स्वर्ग और नर्क में है, उन्हें भी उन जगहों की सहूलियत का फर्क याद रखते हुए अपनी जिंदगी बेहतर रखनी चाहिए। फिर यह भी है कि आज की बात तो एक अकेले वैज्ञानिक प्रयोग के विश्लेषण को लेकर है जो कि किसी और मकसद से किया जा रहा था, और जिसमें कोई और बातें दर्ज हो गईं, आगे चलकर हो सकता है कि विज्ञान कई दूसरे किस्म के नतीजों पर पहुंचने लगे, और यह साबित होने लगे कि आज के किए हुए अच्छे या बुरे काम का कल क्या नतीजा हो सकता है, कल उसका कैसा फर्क पड़ सकता है। विज्ञान अंधाधुंध रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और जो बातें अब तक सिर्फ विज्ञान कथाओं में होते आई हैं, हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में वे हकीकत भी बन जाएं। अभी-अभी 2022 के पहले पचास दिनों की वैज्ञानिक कामयाबियों को लेकर बनाई गई एक लिस्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि महज इतने ही दिनों में विज्ञान ने यह देखा कि परमाणु टेक्नालॉजी में एक बड़ी खोज हुई है जिससे साफ-सुथरी ऊर्जा में मदद मिलेगी, पहली बार एक महिला एचआईवी के इलाज से ठीक हुई है, एमआईटी के इंजीनियरों ने एक नया ऐसा असंभव-पदार्थ बनाया है जो स्टील से अधिक मजबूत है लेकिन प्लास्टिक से भी हल्का है, एंटीबायोटिक के खिलाफ बदन में बनने वाले प्रतिरोध से निपटने में एक बड़ी कामयाबी हुई है, हवा से कार्बन कैद करने की एक बड़ी तकनीक 2022 में ही तैयार हुई है, अब डीएनए तकनीक में इतनी रफ्तार आ गई है कि वह इंसानी जीनोम कुल पांच घंटे दो मिनट में कर ले रही है, रीढ़ की हड्डी में अभी एक ऐसा इम्प्लांट लगाया गया है जिससे लकवाग्रस्त लोग फिर से चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, और तैर रहे हैं, एक इंसान को जानवर का हृदय प्रत्यारोपित किया गया है, 25 बरस की मेहनत से और 10 बिलियन डॉलर की लागत से बनाए गए एक अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने अपनी पहली तस्वीरें दी हैं, स्वीडन के वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा से कार्बनडाइऑक्साइड को ईंधन में बदलने की तकनीक विकसित की है। ये सारी कामयाबियां 2022 से पहले पचास दिनों की हैं, और यह मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि ऐसी तकनीक किसी भी दिन सामने आ सकती हैं जो ये साबित करें कि आज के अच्छे या बुरे काम का नफा या नुकसान कल किस तरह दर्ज हो सकता है। इसलिए एक वैज्ञानिक प्रयोग से निकली हुई एक दार्शनिक किस्म की बात की भावना को समझने की जरूरत है, और उसके मुताबिक अपनी भावनाओं को बदलने की, ताकि अपनी जिंदगी के आखिरी पल सुख देने वाले हों, न कि छाती पर बोझ बनने वाले। और अगले किसी वैज्ञानिक प्रयोग के नतीजे जिंदगी के आखिरी पलों के पहले की पूरी जिंदगी को भी किसी तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसलिए आज से ही अपने तौर-तरीकों को बेहतर बनाने की जरूरत है।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)