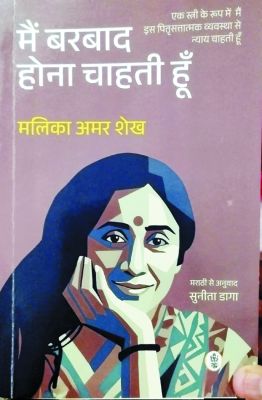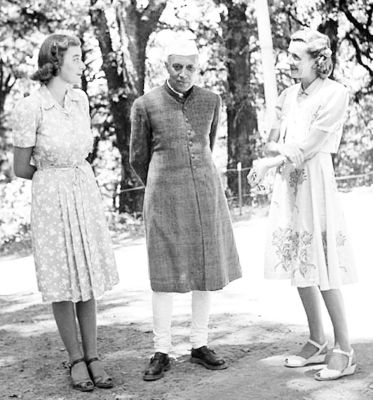विचार / लेख

-संजीव कुमार
वह रोज की तरह अपनी किराने की दुकान बंद करके गली में थोड़ी देर टहलने निकले ही थे कि पीछे से एक मासूम सी आवाज आई — ‘अंकल... अंकल...’
वे पलटे। एक लगभग 7-8 साल की बच्ची हांफती हुई उनके पास आ रही थी।
‘क्या बात है... भाग कर आ रही हो?’ उन्होंने थोड़े थके मगर सौम्य स्वर में पूछा।
‘अंकल पंद्रह रुपए की कनियाँ (चावल के टुकड़े) और दस रुपए की दाल लेनी थी...’ बच्ची की आंखों में मासूमियत और ज़रूरत दोनों झलक रहे थे।
उन्होंने पलट कर अपनी दुकान की ओर देखा, फिर कहा —
‘अब तो दुकान बंद कर दी है बेटा... सुबह ले लेना।’
‘अभी चाहिए थी...’ बच्ची ने धीरे से कहा।
‘जल्दी आ जाया करो न... सारा सामान समेट दिया है अब।’ उन्होंने नर्म मगर व्यावसायिक अंदाज़ में कहा।
बच्ची चुप हो गई। आंखें नीची कर के बोली —
‘सब दुकानें बंद हो गई हैं... और घर में आटा भी नहीं है...’
उसके ये शब्द किसी हथौड़े की तरह उनके सीने पर लगे।
वे कुछ देर चुप रहे। फिर पूछा, ‘तुम पहले क्यों नहीं आई?’
‘पापा अभी घर आए हैं... और घर में...’ वो रुकी, शायद आँसू रोक रही थी।
उन्हें कुछ और पूछने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने बच्ची की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे, ताले की चाबी जेब से निकाल ली। दुकान का ताला खोला, अंदर घुसे, और समेटे हुए सामान को हटाते हुए कनियाँ और दाल बिना तोले ही थैले में डाल दी।
बच्ची ने थैला पकड़ते हुए कहा-‘धन्यवाद अंकल...’
‘कोई बात नहीं। अब घर ध्यान से जाना।’
इतना कह कर उन्होंने दुकान फिर से बंद कर दी।
उस रात वह जल्दी सो नहीं पाए। मन में बच्ची की उदासी, उसका मासूम चेहरा और वो शब्द ‘घर में आटा भी नहीं है...’ गूंजते रहे।
उन्हें अपना बचपन याद आ गया।
वे भी कभी ऐसे ही हालात से गुजरे थे। पिता रिक्शा चलाते थे, मां दूसरों के घरों में काम करती थीं। कई बार तो रात को पानी में रोटी भिगो कर खाना पड़ता था। तब किसी ने मदद की होती तो कितना सुकून मिलता था।
‘अब मेरे पास दुकान है, कमाई है, लेकिन क्या मैंने इंसानियत भी कमा ली है?’ उन्होंने खुद से सवाल किया।
सुबह जब उन्होंने दुकान खोली, तो सबसे पहले एक बोर्ड बनाया— ‘यदि आपको ज़रूरत हो और पैसे न हों, तो बेहिचक बताइए। कुछ सामान उधार नहीं, हक़ से मिलेगा।’
पास में ही एक डब्बा रख दिया, जिस पर लिखा था—
‘अगर आप किसी के लिए मदद करना चाहें, तो इसमें पैसे डाल सकते हैं।’
गली के लोग पहले तो हैरान हुए। लेकिन धीरे-धीरे लोग समझने लगे कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं, ये उस इंसान का दिल था जो अपने अतीत से सबक लेकर किसी का आज सुधारना चाहता था
एक हफ्ते बाद वही बच्ची फिर से आई, इस बार अपने छोटे भाई के साथ।
‘अंकल, पापा ने कुछ पैसे दिए हैं... पिछली बार जो आपने दिया था उसका भी जोड़ लें।’ वह मासूमियत से बोली।
‘नहीं बेटा, उस दिन जो दिया था वो इंसानियत का कजऱ् था। उसका कोई हिसाब नहीं होता।’
बच्ची मुस्कुरा दी। उसने दुकान में रखा वो बोर्ड पढ़ा और बोली — ‘पापा ने कहा है कि जब वे मज़दूरी करके लौटेंगे, तो इस डब्बे में पैसे डालेंगे... ताकि किसी और को भी मदद मिल सके।’
उस दिन उस दुकानदार की आंखें भर आईं। किसी ने सच ही कहा है—‘नेकी कभी बेकार नहीं जाती।’
धीरे-धीरे इस दुकान का नाम गली में फैलने लगा- ‘इंसानियत वाली दुकान।’
गली की बुज़ुर्ग महिलाएं, अकेले रहने वाले बुज़ुर्ग, और दिहाड़ी मज़दूर अब यहां से इज़्ज़त से सामान लेते।
जो सक्षम होते, वे उस डब्बे में कुछ न कुछ डालते जाते।
कई स्कूल के बच्चे भी अपनी गुल्लक से पैसे लाकर उसमें डालते।
यह दुकान अब सिर्फ व्यापार का स्थान नहीं थी, यह एक भरोसे का मंदिर बन गई थी।
कुछ ही समय में इस दुकान की चर्चा सोशल मीडिया पर हुई। एक स्थानीय पत्रकार ने इस कहानी को अपने अख़बार में छापा—
‘जहां मुनाफा जरूरी नहीं, ज़रूरत की कीमत ज़्यादा है-पढि़ए इस दुकान की कहानी’
यह लेख वायरल हो गया। कई सोशल मीडिया पेजों ने इस दुकान का वीडियो बनाया। लोग दूर-दूर से इस ‘इंसानियत वाली दुकान’ को देखने आने लगे।
पर दुकानदार ने कभी उसका फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने कहा—
‘अगर एक बच्ची की भूख ने मुझे बदल दिया, तो शायद ये दुकान किसी और को भी बदल दे।’
वो बच्ची अब रोज स्कूल जाती है। दुकानदार ने उसके स्कूल की फीस भी गुप्त रूप से भर दी।
उसके पिता ने दुकानदार से कहा —
‘आपने उस दिन सिर्फ चावल और दाल नहीं दी थी, आपने मेरी बेटी को भरोसा दिया था कि दुनिया में अच्छे लोग अब भी जि़ंदा हैं।’
आज भी उस दुकान के बाहर वो बोर्ड लगा है —
‘यदि आपको ज़रूरत हो और पैसे न हों, तो बेहिचक बताइए।’
और उस डब्बे में हर दिन कोई न कोई चुपचाप कुछ न कुछ डालकर चला जाता है।
यह कहानी उस छोटी सी बच्ची की है, लेकिन यह बदलाव की बड़ी लहर बन चुकी है।
एक व्यक्ति, एक दुकान, और एक मासूम सी आवाज़ ने यह सिद्ध कर दिया कि—
‘बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, दिल के भीतर से होती है।’
(फेसबुक)