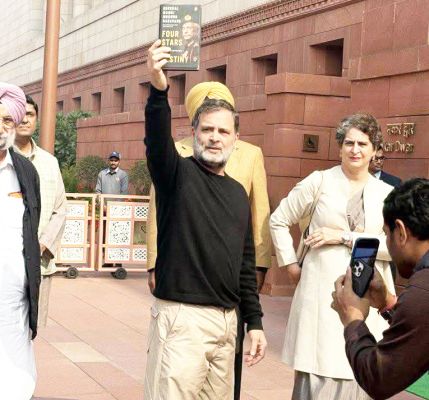विचार / लेख

जाने-माने लेखक, स्तंभकार और ग्लोबल इनवेस्टर रुचिर शर्मा का मानना है कि मौजूदा समय में भारतीय अर्थव्यवस्था चीन के मुक़ाबले पिछड़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर किसी को एक समान मौके दिए जाने की ज़रूरत है।
उन्होंने ये भी कहा कि लोगों के लिए कल्याण संबंधी योजनाओं और कॉरपोरेट संबंधी योजनाओं में संतुलन करने की ज़रूरत है।
बीबीसी हिंदी के संपादकों और पत्रकारों से पिछले दिनों रुचिर शर्मा ने एक लंबी बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था, अमेरिका-चीन की आपसी होड़, भारतीय अर्थव्यवस्था और नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं पर विस्तार से अपनी बात रखी।
रुचिर शर्मा 2002 से अमेरिकी शहर न्यू यॉर्क में रह रहे हैं। वह उन भारतीयों में हैं, जिन्होंने अमेरिका में जाकर अपना एक मुकाम बनाया है।
ट्रंप की वापसी से भारत को नफा या नुकसान?
डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर वापसी से भारत को कितना फ़ायदा होगा, पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘ट्रंप की मानसिकता रणनीतिक न होकर लेन-देन वाली है। इसलिए उनका ध्यान इसपर रहेगा कि वह भारत के साथ कैसा व्यापार कर सकते हैं। अगर भारत चीन के साथ कोई व्यापार संधि कर रहा है तो उसमें अमेरिका की क्या हिस्सेदारी रहेगी। तो कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच रिश्ते लेन-देन आधारित रहने वाले हैं।’
आम भारतीयों की दिलचस्पी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के आपसी रिश्तों में भी है, क्या इसका कोई फ़ायदा भारत को नहीं होगा, पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘मित्रता का फायदा होता है। लेकिन ट्रंप के लिए लेन-देन ही सबसे अहम चीज़ है। ट्रंप को जो लोग जानते हैं उनका कहना है कि ट्रंप का कोई दोस्त नहीं है, उनकी केवल लोगों से जान-पहचान है।’
‘उनके पास कोई असली दोस्त नहीं है। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उनकी जान-पहचान बहुत लोगों से हैं, लेकिन उनका कोई नज़दीकी दोस्त नहीं है। इसलिए अगर कोई ये मानता है कि ट्रंप उनके दोस्त है और इससे उन्हें कोई फायदा होगा, तो ऐसा होना मुश्किल है।’
राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में क्या बदलाव आएंगे और ट्रंप को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? इस पर रुचिर शर्मा कहते हैं, ‘आज का अमेरिका दो दिशा में जा रहा है। एक तरफ़ आपको ये सुनने को मिलेगा कि अमेरिका में बहुत राजनीतिक ध्रुवीकरण है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में बहुत दुश्मनी है। साथ ही, वहां के सर्वे भी इसी बात को दिखाते हैं कि वहां के नागरिक देश की स्थिति से काफी नाखुश है। वहां हर औसत अमेरिकन को लगता है कि अमेरिका का सिस्टम लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है।’
‘दूसरी तरफ़ यह कि दुनियाभर का सारा पैसा अमेरिका को ही जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि डॉलर की कीमत रुपये और दूसरी करेंसी के मुकाबले काफी ज्यादा है। ट्रंप के आने के बाद इसमें और गति आई है। मुझे नहीं पता कि ट्रंप कैसे इस विरोधाभास को संभाल पाएंगे कि एक तरफ़ तो अमेरिका इतना पैसा जा रहा है, स्टॉक मार्केट इतना बढ़ रहा है, डॉलर की कीमत इतनी बढ़ रही है। साथ ही, अमेरिका एआई के मामले में काफी मजबूत स्थिति में हैं।’
पूंजीवाद और लोकतंत्र पर क्या बोले?
रुचिर शर्मा अपनी किताब ‘व्हाट वेंट रांग विद कैपिटलिज़म’ में कहते हैं कि पूंजीवाद को मजबूत करने के लिए लोकतंत्र का होना ज़रूरी है।
इस पहलू पर वह कहते हैं, ‘पूंजीवादी देशों में सरकार की भूमिका बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए इसको पूंजीवाद कहना ठीक नहीं होगा। क्योंकि पूंजीवादी देशों में व्यक्ति की आर्थिक आजादी पर कोई बंदिशे नहीं होती है। लेकिन अगर सरकार की भूमिका इतनी बढ़ गई है कि सरकार व्यापार पर इतने नियम लगा रही है, बड़ी-बड़ी कंपनियों को मदद कर रही है, कंपनियों को राहत पैकेज देकर उन्हें बिखरने से रोक रही है। इसलिए पश्चिमी समाज में पूंजीवाद की परिभाषा बदल गई है।’
हालांकि पिछले कुछ सालों में लोकतांत्रिक देशों में आंतरिक तौर पर ख़तरा बढ़ा है।
रुचिर शर्मा से जब पूछा गया कि जिन देशों में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, वहां पूंजीवाद का फैलना लोगों के लिए कितना सुरक्षित होगा तो उन्होंने कहा, ‘यह कहना बिल्कुल ठीक है कि लोकतांत्रिक देशों को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन अगर आप चीन को भी देखे, तो वहां भी पिछले पांच-दस सालों में काफी समस्या आई है।’
‘तो यह कहना कि अगर सत्तावादी सरकार के आने से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, तो चीन इस बात का उदाहरण है कि ऐसा नहीं होता है। अगर आपके शीर्ष नेतृत्व के नेता कोई गलती करते हैं, जैसे चीन में शी-जिनपिंग ने काफी गलतियां की, तो इससे भी अर्थव्यवस्था डूब सकती है।’
पूंजीवाद और समाजवाद, दोनों आर्थिक नीतियों में कौन सी प्रणाली ज़्यादा बेहतर है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘जिस पूंजीवाद को आज हम पश्चिमी देशों में देखते हैं, वह सच्चा पूंजीवाद नहीं है। पूंजीवाद की नींव रखने वाले दार्शनिक अगर आज के पूंजीवाद को देखेंगे तो वह कहेंगे कि यह तो पूंजीवाद नहीं है। पूंजीवादी प्रणाली में हम बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वहां लोगों को ज़्यादा आजादी मिले।’
चीन कैसे भारत से आगे?
रुचिर शर्मा का ये भी मानना है कि पूंजीवाद गऱीबों की हक की बात करता है। उन्होंने ये भी बताया कि 1960 और 1970 तक चीन पूरा समाजवाद पर आधारित था।
1970 के बाद चीन ने पूंजीवाद को अपनाना शुरू किया और उसके बाद हमने देखा कि चीन में कितना विकास हुआ। लेकिन अहम सवाल यह है कि पिछले सौ सालों में पूरी दुनिया में आदर्श पूंजीवाद का कोई उदाहरण देखने को मिला है?
इस पर रुचिर शर्मा ने कहा, ‘मैंने अपनी किताब में तीन देशों का जि़क्र किया है, जहां पर पूंजीवाद आज काम कर रहा है। सबसे पहला देश स्विट्जरलैंड है। स्विट्जऱलैंड आज सबसे अमीर देशों में से एक है। उनकी प्रति व्यक्ति आय अमेरिका से भी ज़्यादा है।’
‘इसके अलावा मैंने ताइवान और वियतनाम का उदाहरण दिया है। वियतनाम भी पहले एक समाजवाद को मानने वाला राज्य था। फिर उन्होंने पिछले 20-30 सालों में अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत उदार किया है। आज के समय में वियतनाम में फॉरेन डायेरेक्ट इनवेस्टमेंट भारत से भी ज्यादा जा रहा है।’
भारतीय संदर्भ में रुचिर शर्मा ने कहा, ‘भारत में सरकार की भूमिका बहुत ज्यादा रही है। व्यापार के समर्थन में होना और पूंजीवाद को समर्थन देना, ये दोनों दो अलग-अलग चीजें होती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत में ज्यादातर पॉलिसी कुछ लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, जिनमें बड़े-बड़े उद्योगपतियों की भूमिका ज्यादा रहती है।’
‘मैं यह कहता रहा हूं कि सरकार छोटे और मध्यम व्यापार को काफी आजादी दें। लेकिन भारत में इतने सारे नियम हैं कि व्यापार करना मुश्किल हो जाता है। हमें यह अंतर समझने की जरूरत है कि पूंजीवाद के समर्थन में होना और बड़े व्यापार के समर्थन में होने में काफ़ी बड़ा अंतर होता है।’
भारत में नरेंद्र मोदी सरकार के लगातार तीसरी बार चुने जाने की वजहों के बारे में रुचिर शर्मा ने बताया, ‘पिछले 5-10 सालों में भारत में विरोधी लहर में काफी कमी आई है और अब 50 प्रतिशत से ज्यादा सरकारें दोबारा चुनाव जीतकर वापस सत्ता में आ रही हैं।’
‘सबसे महत्वपूर्ण बदलाव भारत के डिजिटल इनफ्रास्ट्रक्चर में आया है। इसके कारण लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। 1980 के दशक में राजीव गांधी का एक बयान था कि सरकार 1 रुपये खर्च करती है तो लोगों तक केवल 15 पैसे ही पहुंचते हैं। लेकिन अब इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। पिछले 5-10 सालों में सरकार अगर कुछ पैसे लोगों को भेजती है, तो काफी पैसा सीधे लोगों तक पहुंचता है। हमने महाराष्ट्र और हरियाणा में भी देखा कि आखिर में काफी पैसा लोगों तक पहुंचा, जिसके कारण सरकार दोबारा चुनकर आई।’
मुफ्त के वादों से क्या असर?
राजनीतिक दल एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बढ़-चढक़र योजनाओं (रेवडिय़ों) की घोषणा करती है।
रुचिर शर्मा से ये पूछा गया कि उनके मुताबिक ये रेवड़ी क्या है और क्या ये एक टिकाऊ मॉडल हो सकता है? इसके जवाब में उन्होंने कहा, ‘ये एक टिकाऊ मॉडल नहीं है। इसे हम दो देशों के उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ़ 1970 तक बहुत लोग इस बात को कहते थे कि ब्राजील आने वाले समय में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर सामने आएगा। वहीं दूसरी तरफ़ चीन 1970 में काफी पिछड़ा हुआ था।’
‘ब्राजील 1980 और 1990 के दशक में अपने आप को एक कल्याणकारी राज्य बनाने में जुटा हुआ था। उन्होंने इसके लिए बहुत पैसा खर्च किया। जिसके कारण 1980 के बाद से उनकी विकास दर दो प्रतिशत पर आकर अटक गई और कर्जा भी बहुत बढ़ गया। वहीं चीन में सरकार की भूमिका को आर्थिक मामलों में कम करना शुरू किया गया। 1990 में चीन ने 10 करोड़ लोगों को पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से निकाल दिया और लोगों को कोई भी कल्याणकारी योजना देने से मना कर दिया। भारत भी इन दो देशों के मॉडल से कुछ सीख सकता है।’
‘भारत में एक निवेशक के तौर पर मेरे लिए सबसे बड़ा जोखिम यह है कि भारत ने पिछले 5-7 सालों में जो संतुलन बनाया था, वह अब बिगडऩे लगा है। क्योंकि अब सरकार कल्याणकारी योजना पर ज्य़ादा खर्च करेगी और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर कम पैसा खर्च करेगी। इसके कारण हमारी विकास दर चीन की तरह कभी देखने को नहीं मिलेगी।’
मनरेगा की फंडिंग घटने से क्या असर?
भारत में मनरेगा एक ऐसी व्यवस्था है, जो गरीबों के हितों के लिए काम करती है। लेकिन सरकार ने मनरेगा की फंडिंग को कम कर दिया तो दूसरी तरफ अमीर लोगों को राहत पैकेज दिया जा रहा है।
इस पहलू पर रुचिर शर्मा का मानना है, ‘मैं राहत पैकेज दिए जाने के बिल्कुल खिलाफ हूं। अमेरिका में एक लंबे समय तक निजी सेक्टर की कंपनियों को राहत पैकेज नहीं दिया जाता था। लेकिन अमेरिका में 1980 में इसमें काफी तेजी आई है।’
भारतीय अर्थव्यवस्था के चीन की तरह 9 से 10 प्रतिशत की विकास दर से आगे बढऩे के लिए रुचिर शर्मा कुछ सुझाव भी देते हैं।
वह कहते हैं, ‘आप को चीन की तरह 9 से 10 प्रतिशत की विकास दर से आगे बढऩा है, तो आपको यह समझना होगा कि चीन ने इसके लिए क्या किया। चीन ने कहा कि हम 9 से 10 प्रतिशत की विकास दर से आगे बढ़ेंगे और इससे ही ज्य़ादा से ज़्यादा लोगों को मदद की जा सकेगी। जीवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत नतीजों की समानता नहीं है यानी सभी लोगों को एक जैसा परिणाम मिले। लेकिन इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत है मौकों की समानता देना, जहां सभी लोगों को समान मौका मिले।’
अमेरिका में एक बात कही जाती है कि वहां कोई भी जाकर सफल हो सकता है, लेकिन क्या ये बात आज के समय में भी पूरी तरह से ठीक है?
इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘नहीं इसमें काफी बदलाव आया है। अगर आप सर्वे का डेटा देखे तो अमेरिका में 50 साल पहले 80 प्रतिशत लोग इस बात को कहते थे कि हमारी जिंदगी हमारे माता-पिता से ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन आज ये बात केवल 30 प्रतिशत लोग ही कहते हैं। तो अमेरिका में काफी बदलाव आया है। लेकिन फिर भी अमेरिका में अभी काफी कुछ अच्छा है, जिसके कारण अमेरिका अब भी सभी आप्रवासियों का मनपसंद ठिकाना बना हुआ है।’
आज के समय में दुनियाभर में भारत को लेकर धारणा के बारे में उन्होंने कहा, ‘अमेरिका में एक चीज़ लोग काफी बोलते हैं कि भारतीयों का ब्रांड वैल्यू काफी बढ़ा है। ये वाकई में सच बात है कि भारतीय ब्रांड काफी मजबूत है। अमेरिका में लोग इस बात को देखते हैं कि वहां की बड़ी-बड़ी कंपनियों के ज्य़ादातर सीईओ तो भारतीय ही हैं। इस बात को मानते हैं कि भारतीय लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। अब सरकार इसका अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें तो ये दूसरी बात है। लेकिन फिर भी ज्यादातर निवेशक भारत को व्यापार करने के लिए मुश्किल देश मानते हैं।’
अमेरिका के टैरिफ़ से भारत संग कारोबार पर असर
अफ्रीका और एशिया में बहुत सारे देशों का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है और चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट में हैं। ऐसे समय में जब अमेरिका टैरिफ़ बढ़ा सकता है, तो ये भारत जैसे देशों में कारोबार के लिहाज से कैसे रहने वाला है?
इस बारे में रुचिर शर्मा ने कहा, ‘भारत को भी अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए और खासकर अपने पड़ोसी देशों के साथ। ज्यादातर सफल देश अपने पड़ोसियों के साथ काफी व्यापार करते थे। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद उन्होंने आसपास के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने पर काफी ध्यान दिया था।’ ‘लेकिन फिर भी पिछले 11 सालों में यह व्यापार ज्य़ादा बढ़ा नहीं है। वहीं आप दुनिया में देखे तो पड़ोसियों के साथ सबसे कम व्यापार दक्षिण एशिया में हुआ है।’
भारत में 2011 के बाद से सामाजिक-आर्थिक जनगणना नहीं हुई है। सरकार पर बहुत बार यह आरोप लगता है कि वह बहुत सारे महत्वपूर्ण डेटा को जारी नहीं कर रही है।
यह आरोप भी लगता है कि डेटा को इस तरीके से बनाया जा रहा है, जिससे भारत की तस्वीर अच्छी दिखें।
इन आरोपों पर रुचिर शर्मा ने बताया, ‘भारत का डेटा सिस्टम काफी खराब है। इसे हर प्रकार से ठीक करने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि ये समस्या प्रोपेगेंडा के साथ-साथ अयोग्यता की भी है। वित्तीय दुनिया में निवेशक सरकार के डेटा से ज्यादा अपने इंडिकेटर पर ध्यान देते हैं। तो हम सरकार के डेटा पर इतना भरोसा नहीं करते हैं।
क्या आने वाले दिनों में वैश्विक बाज़ार में अमेरिकी दबदबा कम होने वाला है, इस सवाल के जवाब में वे कहते हैं, ‘अपनी किताब ‘ब्रेकआउट नेशन’ में मैंने कहा था कि ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था दुनिया पर हावी होगी और अमेरिका का टूटना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज मेरा मानना यह है कि निवेश की दुनिया में सारा दबदबा अमेरिका का है।’
‘तो जो बात मैंने 12 साल पहले अपनी किताब में लिखी थी, वह सब ग़लत साबित हो रही है। क्योंकि आज चीन, ब्राजील और बाकी ब्रिक्स देशों में काफी आर्थिक मंदी है और सभी निवेशकों को अमेरिका निवेश के लिए अच्छा लग रहा है। लेकिन इसके बाद भी मेरा मानना यही है कि अमेरिका के दबदबे में थोड़ी कमी आएगी। इसलिए मेरी सलाह यही है कि सारा पैसा एक मार्केट में न लगाकर अमेरिका के बाहर वाली मार्केट में भी लगाएं।’ (bbc.com/hindi)