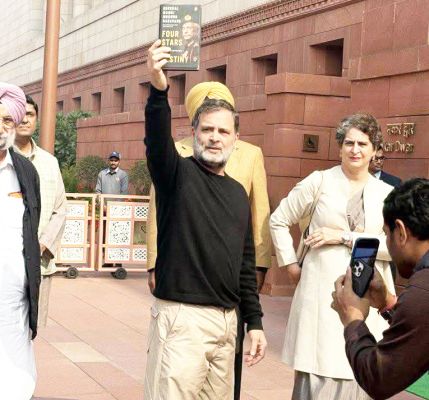विचार / लेख
-उमंग पोद्दार
जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 10 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर होने जा रहे हैं। हाल के वर्षों में देश के सबसे प्रभावशाली मुख्य न्यायाधीशों में से एक रहे जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल की कई वजहों से आलोचना हो रही है।
लोगों को उनसे उम्मीदें थीं कि वो सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज का तरीक़ा बदलेंगे, आम नागरिकों के लिए इंसाफ़ हासिल करना आसान बनाएंगे और ‘बहुसंख्यकवादी सरकार’ पर संवैधानिक नियंत्रण रखेंगे।
शायद उनसे उम्मीदें ही इतनी ज़्यादा थीं कि न्यायपालिका पर नजऱ रखने वाले बहुत से लोग चीफ़ जस्टिस के तौर पर उनके कार्यकाल को निराशा के साथ देख रहे हैं।
उनके न्यायिक फ़ैसलों के साथ-साथ उनके निजी बर्ताव पर भी चर्चा हो रही है। जस्टिस चंद्रचूड़, अपने भाषणों और इंटरव्यू से मीडिया की सुर्खय़िों में बने रहे, ऐसा इतिहास में उनसे पहले शायद ही देखा गया हो।
क्यों हो रही आलोचना?
हाल की दो बातों की वजह से एक न्यायाधीश के तौर पर उनके व्यवहार की आलोचना की गई।
पहला तो उन्होंने कहा कि जब अयोध्या मामले की सुनवाई चल रही थी, तो उन्होंने ‘भगवान के सामने बैठकर मदद की गुहार’ लगाई थी।
दूसरा विवाद उस समय पैदा हुआ, जब जस्टिस चंद्रचूड़ के घर पर गणेश पूजा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो वायरल हुआ।
ये दोनों ही बातें ऐसी थीं जिनकी न्यायाधीशों से उम्मीद नहीं की जाती है। पहला, अपने फ़ैसलों का जनता के बीच बचाव करना, दूसरा, किसी धार्मिक आयोजन में राजनीतिक नेतृत्व से जुड़े लोगों से मिलना।
अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में जस्टिस चंद्रचूड़ गणेश पूजा को एक च्निजी आयोजनज् बताया और कहा कि इसमें च्कुछ भी ग़लत नहींज् था।
इन कुछ घटनाओं के अलावा, जस्टिस चंद्रचूड़ अपने पीछे एक पेचीदा विरासत छोडक़र जा रहे हैं। ऐसे में उनके कार्यकाल को स्पष्ट रूप से किसी खांचे में रख पाना मुश्किल है।
जस्टिस चंद्रचूड़ ऐसे कई मक़सद हासिल करने में असफल रहे, जो ख़ुद उन्होंने अपने लिए तय किए थे।
लेकिन उन्होंने ऐसे भी कई फ़ैसले सुनाए, जो सरकार के दबदबे के ख़िलाफ़ थे और जिनसे जनता के अधिकारों का दायरा बढ़ा,
मगर साथ ही चंद्रचूड़ ने ऐसे भी कई निर्णय दिए, जिनसे नागरिकों के अधिकारों पर ऐसा असर पड़ा जिसे कई लोग प्रतिकूल मानते हैं।
जस्टिस चंद्रचूड़ के कुछ फ़ैसलों ने भविष्य के लिए एक आदर्शवादी बुनियाद रखी, लेकिन उनमें से कई मामलों में वो फ़ौरी तौर पर कोई राहत नहीं दे सके।
इसके अलावा, सरकार पहले की तरह लगातार न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए दबाव डालती रही और राजनीतिक रूप से संवेदनशील कई मामलों की लिस्टिंग को लेकर भी उनकी आलोचनाएं हुईं।
‘मास्टर ऑफ दि रोस्टर’ के तौर पर जस्टिस चंद्रचूड़ का व्यवहार
एक जज के तौर पर जस्टिस चंद्रचूड़ शांत रहकर हर वकील को पूरे धैर्य से अपनी बात कहने का मौक़ा देने के लिए जाने जाते थे। भले ही वकील सीनियर हों या नहीं।
भारत में न्यायपालिका के शिखर पर बैठने वाले चीफ़ जस्टिस के पास बहुत व्यापक अधिकार होते हैं।
वो ‘मास्टर ऑफ दि रोस्टर’ होते हैं। उनके पास ये तय करने का पूरा अख़्तियार होता है कि किसी केस की किस बेंच के सामने सुनवाई हो। कौन से जज किस मामले को सुनें।
अक्सर किसी केस के फ़ैसले पर इस बात का असर होता है कि उसकी सुनवाई कौन से जज कर रहे हैं।
कुछ जज रूढि़वादी होते हैं, वहीं कुछ उदारवादी होते हैं और अक्सर न्यायाधीशों के इन वैचारिक झुकावों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में घूमने वालों को पता होता है।
ऐसे में मुख्य न्यायाधीश ‘मास्टर ऑफ दि रोस्टर’ की ताक़त का इस्तेमाल करके, कुछ मामलों के अंतिम निर्णय को भी प्रभावित कर सकते हैं।
2017 में जब जस्टिस दीपक मिश्रा मुख्य न्यायाधीश थे, तो सुप्रीम कोर्ट के चार जजों की एक बेंच ने एक ऐतिहासिक प्रेस कांफ्रेंस की, और ये शिकायत की थी कि मुख्य न्यायाधीश राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों को कुछ चुनिंदा बेंचों को ही आवंटित कर रहे हैं।
तब से ही ये एक संवेदनशील विषय माना जाता रहा है कि किस मामले की सुनवाई किस बेंच में होगी।
जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल में भी कुछ अहम मामलों की किसी ख़ास बेंच के सामने लिस्टिंग की आलोचना हुई।
जब वो चीफ़ जस्टिस बने थे, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अदालतों को और पारदर्शी बनाना चाहते हैं।
हालांकि, जब अहम मुक़दमों की लिस्टिंग का सवाल आया, तो उनकी ये बात व्यावहारिक तौर पर पूरी तरह लागू होती नहीं दिखी।
कार्यकाल की एक अहम बात
उनके कार्यकाल की एक अहम बात ये रही कि संविधान पीठ से जुड़े 33 मामलों का निपटारा हुआ।
ये वो मामले हैं, जो क़ानून के व्यापक प्रश्नों से जुड़े थे, और उनके लिए पांच या फिर उससे भी ज़्यादा जजों की बेंच की ज़रूरत थी।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 370 ख़त्म करने जैसे कई अहम मामलों की सुनवाई के लिए 5, 7 और 9 जजों की बेंच का गठन किया।
संविधान पीठ के गठन के मामले में कुछ मुक़दमों को दूसरों के ऊपर तरजीह देने पर भी सवाल उठे। मसलन, समलैंगिक जोड़ों की शादी से जुड़े मामले।
चंद्रचूड़ उन बेंचों में शामिल रहे थे, जिसने निजता के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया था और समलैंगिकता को अपराध मानना ख़त्म किया था।
इसी वजह से उनसे बड़ी उम्मीदें थीं कि अब वो समलैंगिकों के शादी करने के अधिकार के मसले पर भी ध्यान देंगे। ये मामला लिस्ट हुआ और रिकॉर्ड तेज़ी के साथ इसे पांच जजों की बेंच के हवाले कर दिया गया।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में चल रहे ऐसे सारे मामले अपने पास मंगा लिए, हालांकि समलैंगिक समुदाय के लिए इस मामले का आखऱिी नतीजा वैसा नहीं निकला, जिसकी उन्हें उम्मीद थी।
सभी पांच जजों ने आम राय से ये फ़ैसला दिया कि विवाह करना कोई बुनियादी अधिकार नहीं है।
वैसे तो कुछ मामलों की सुनवाई बड़ी तेज़ी से हुई पर दूसरे कई अहम माने जाने वाले मामले अदालत में लटके रहे।
मिसाल के तौर पर नागरिकता संशोधन क़ानून से जुड़े मामले और शादीशुदा जि़ंदगी में रेप का सवाल।
जमानत के मामले
नागरिकों की स्वतंत्रता के कुछ मामलों में जस्टिस चंद्रचूड़ ने बड़ी तेज़ी दिखाई।
मिसाल के तौर पर जब सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात हाई कोर्ट ने ज़मानत देने से इनकार कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार के दिन विशेष सुनवाई करके ज़मानत दी थी।
लेकिन, जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल में ही भीमा कोरेगांव मामले के अभियुक्त महेश राउत पिछले पांच साल से भी ज़्यादा वक़्त से जेल में बंद हैं।
इस मामले में 16 कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी जाति पर आधारित हिंसा को बढ़ावा देने और प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) से रिश्तों के आरोप में जेल में बंद हैं।
2023 में महेश राउत को बॉम्बे हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी, फिर भी उनकी ज़मानत पर रोक लगा दी गई और मामला अब तक सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है।
आमतौर पर हाई कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक नहीं लगाता है, लेकिन ये मामला जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच में अब तक अटका हुआ है।
आलोचक तो यहां तक कहते हैं कि ये मामला दो जजों की एक बेंच के सामने सुनवाई के लिए लिस्ट हुआ था, जिसमें जूनियर जज के तौर पर जस्टिस बेला त्रिवेदी भी शामिल थीं।
लेकिन, लिस्टिंग के नियमों के उलट ये मामला उस बेंच में चला गया जहां बेला त्रिवेदी सीनियर जज थीं।
ज़मानत से जुड़ा एक और मामला उमर ख़ालिद का है, जो दिल्ली दंगों में अभियुक्त हैं। वो पिछले चार साल से ज़्यादा वक़्त से जेल में बंद हैं।
जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच में सुनवाई से पहले उनका केस पहले दूसरी बेंचों में भी लिस्ट हुआ था।
एक और मामला ऋतु छाबडिय़ा का है। ऋतु छाबडिय़ा के मामले में दो जजों की एक बेंच ने कहा था कि अधूरी चार्जशीट दायर करना, अपने आप ही ज़मानत का आधार बन जाता है।
सिफऱ् मौखिक रूप से उल्लेख किए जाने पर दो जजों की बेंच में बैठे जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस मामले को अपनी बेंच में ट्रांसफर कर लिया और आखऱि में इस आदेश पर स्टे लगा दिया।
न्यायिक नियमों के ख़िलाफ़ बताते हुए उनके इस फ़ैसले की आलोचना की गई थी। ये मामला अब तक सर्वोच्च अदालत में लंबित है।
सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने चीफ़ जस्टिस के तौर पर चंद्रचूड़ के कार्यकाल के बारे में लिखा, ‘बेंचों के गठन और मामलों के आवंटन के मामले में बहुत कमियां देखने को मिलीं।’
ऐसे कई और उदाहरण हैं जिनमें मुक़दमों की लिस्टिंग नहीं होने से नागरिकों की स्वतंत्रता और सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही को लेकर सवाल उठे।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की समीक्षा के लिए दायर की गई याचिका भी चंद्रचूड़ के कार्यकाल में अटकी रही जबकि सरकार के आलोचकों और विपक्ष के ख़िलाफ़ इस क़ानून के दुरुपयोग का इल्ज़ाम लगातार लगता रहा है।
2022 के एक फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ़्तारी, जांच और ज़मानत के विषय में प्रवर्तन निदेशालय को खुली छूट दे दी थी। यहां तक कि ये फ़ैसला होने के बाद इसकी समीक्षा की याचिका दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश अपना नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर कहते हैं, ‘पीएमएलए के मामलों की जिस तरह से सुनवाई हुई, उससे लगा कि अदालत इस मामले में सरकार के रुख़ को स्वीकार करती है।’
उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से ज़मानत के कुछ मामलों की सुनवाई की गई, वो भी ‘चिंताजनक’ है।
एक और मामला जो जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल में पेंडिंग रहा, वो चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के रवैए को लेकर था।
जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था अनिल मसीह ने बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए चुनाव में धांधली की थी। इस साल उनके ख़िलाफ़ अदालत में झूठा बयान देने का मामला शुरू किया गया था।
जब मामले की सुनवाई शुरू हुई, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने अनिल मसीह को फटकारा, इससे लगा कि वो अनिल मसीह को दंडित करेंगे, लेकिन उसके बाद वो मामला कभी सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हुआ।
वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े के मुताबिक़, ‘अगर हम स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल को एक वाक्य में बयां करना चाहें, तो आप ये कह सकते हैं कि उमर ख़ालिद जेल में हैं और अनिल मसीह आज़ाद घूम रहे हैं।’
वैसे तो जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल में संविधान पीठ में पहले से कहीं ज़्यादा मामलों के निपटारे हुए। लेकिन, उनके दौर में लंबित मामलों की संख्या में भी तेज़ी से बढ़ोत्तरी हुई।
जब चंद्रचूड़ ने काम संभाला था, तब 69 हज़ार केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे और अब जबकि वो रिटायर हो रहे हैं, तो लंबित मुक़दमों की तादाद 82 हज़ार तक जा पहुंची है।
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर कहते हैं, ‘मुझे लगता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रशासनिक क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि वो लंबित मामलों में कमी लाएं। मौजूदा चीफ जस्टिस ने संविधान पीठ की चुनौती को तो स्वीकार किया लेकिन, वो लंबित मामलों की तादाद पर क़ाबू कर पाने में नाकाम रहे।’
कॉलेजियम के मुखिया के तौर पर
बहुत से लोग ये कहते हैं कि न्यायिक नियुक्तियों के मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल नाकामी वाला रहा है।
व्यवस्था ये है कि न्यायपालिका की नियुक्तियों में उच्च न्यायपालिका के वरिष्ठ जजों वाले कॉलेजियम की राय अंतिम होती है।
अगर सरकार को कॉलेजियम की ओर से सुझाए गए नामों से दिक़्क़त भी है, तो वो केवल एक बार ही उनको समीक्षा के लिए वापस कॉलेजियम के पास भेज सकती है।
लेकिन अगर कॉलेजियम उस नाम की सिफ़ारिश दोबारा भेजे, तो सरकार को मानना ही पड़ेगा।
पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकारों ने इसका कड़ा विरोध किया है और जजों की नियुक्ति में अपनी बात मनवाने की कोशिश की है।
इसकी वजह से अक्सर न्यायाधीशों की नियुक्ति अटक जाती है, या फिर सरकार की पसंद वाले जज नियुक्त हो जाते हैं।
जब जस्टिस चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश बने, तो उन्होंने ख़ुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका एक लक्ष्य न्यायापालिका के ख़ाली पदों में अलग अलग तबक़ों के जजों की नियुक्ति करना है।
क़ानून के बहुत से जानकारों के बीच इस बात पर मोटे तौर पर सहमति है कि जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल में जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार के दबदबे पर लगाम नहीं लगाई जा सकी।
जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ काम कर चुके सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज ने नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर कहा, ‘वो सरकार पर पर्याप्त दबाव बना पाने में नाकाम रहे हैं। नियुक्ति प्रक्रिया के मामले में ये एक बड़ी समस्या है। सरकार के आगे झुकते रहे।’
सुप्रीम कोर्ट के इन पूर्व जज ने कहा कि चंद्रचूड़ का कार्यकाल काफ़ी लंबा था और उसके पास पर्याप्त समय था कि वो न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका का प्रभुत्व दोबारा क़ायम कर सकते थे।
वे कहते हैं, ‘छोटे कार्यकाल वाले चीफ जस्टिस से आप सरकार के दबाव का विरोध करने की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘हाई कोर्ट बहुत मुश्किल स्थिति में हैं।’
न्यायालयों में 351 पद खाली
जब जस्टिस चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश बने, तो उच्च न्यायालयों में जजों के 323 पद ख़ाली थे, आज दो साल बाद ख़ाली पदों की संख्या बढक़र 351 पहुंच चुकी है।
उनके कार्यकाल का एक मामला ख़ासा दिलचस्प है, सुप्रीम कोर्ट अदालत की अवमानना के एक क़ानूनी पहलू की सुनवाई कर रहा था कि सरकार जजों की नियुक्तियों के मामले में क़ानून का पालन नहीं कर रही है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल कर रहे थे।
सुनवाई के दौरान उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने क़ानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, तो वो सरकारी अधिकारियों को अदालत की अवमानना का दोषी मानेंगे।
जस्टिस कौल के कार्यकाल के आखऱिी दिनों में ये मामला लिस्ट होने के बावजूद सूची से ग़ायब हो गया।
ख़ुद जस्टिस संजय किशन कौल इस बात से हैरान रह गए थे। उन्होंने उस वक़्त कहा था, ‘मैंने इस केस को नहीं हटाया है, कुछ बातों पर मुंह बंद ही रखा जाए, तो बेहतर है। मुझे यक़ीन है कि चीफ़ जस्टिस को इस बात की जानकारी है।’
ये एक विचित्र स्थिति थी क्योंकि जस्टिस संजय किशन कौल ने इस मामले को अपनी बेंच में 5 दिसंबर को लिस्ट करने के लिए कहा था। उसके बाद से इस केस की सुनवाई का अब तक नंबर नहीं आया है।
जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी, तब न्यायपालिका ने केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ सख़्त टिप्पणियां की थीं। जिसके बाद जजों की नियुक्ति के मामले में कुछ प्रगति हुई थी।
यहां तक कि जो नियुक्तियां हुई भी हैं, उनमें से कई जजों को नियुक्त करने और कुछ को हाई कोर्ट का जज नहीं बनाने को लेकर चिंताएं व्यक्त की गईं।
इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हाई कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के लिए ‘कॉलेजियम ने 164 जजों के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिनमें से 137 नियुक्तियाँ हो चुकी हैं, जबकि 27 नामों पर सरकार ने कोई फ़ैसला नहीं लिया है’।
ये मामले चर्चा में रहे
एक मामला मद्रास हाई कोर्ट की एक जज विक्टोरिया गौरी का था। उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ नफऱत भरे बयान दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में एक याचिका भी दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये बात कॉलेजियम के ध्यान में नहीं लाई गई थी। उन्होंने इस मामले की सुनवाई अगले दिन के लिए तय की।
जब सुनवाई हुई, तो एक और बेंच ने कहा कि कॉलेजियम ने जस्टिस विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति सभी बातों को ध्यान में रखते हुए की थी और इस याचिका को ख़ारिज कर दिया गया।
कुछ जजों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें सरकार विरोधी फ़ैसलों की वजह से सुप्रीम कोर्ट में नहीं नियुक्त किया गया।
जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल में ऐसा ही एक मामला जस्टिस मुरलीधर का था। दिल्ली हाई कोर्ट के सबसे सीनियर जजों में से एक जस्टिस मुरलीधर को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने के बजाय उनका तबादला ओडिशा कर दिया गया।
यहां तक कि अहम उच्च न्यायालय माने जाने वाले मद्रास हाई कोर्ट में उनके तबादले पर भी बताया जाता है कि केंद्र सरकार को एतराज़ था, इसके बाद कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफ़ारिश दोबारा नहीं की।
उनको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाने पर क़ानून के तीन बड़े जानकारों ने लेख लिखकर सवाल उठाया कि ‘जस्टिस मुरलीधर को सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं बनाया गया? ख़ासतौर से तब जब सुप्रीम कोर्ट में दो पद ख़ाली थे।’
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर के मुताबिक़, कॉलेजियम व्यवस्था न्यायपालिका की स्वतंत्रता की प्रतीक है।
उन्होंने कहा, ‘आज ऐसा लगता है कि संभावित जजों की कि़स्मत का फ़ैसला सरकार कर रही है।’
एक क्षेत्र जहां जस्टिस चंद्रचूड़ कुछ हद तक कामयाब रहे, वो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का है।
उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में 18 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। हालांकि, ऐसा करते वक़्त उन्होंने विविधता का पैमाना लागू करने का अपना वादा नहीं निभाया। उनके दौर में सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला जज की नियुक्ति नहीं की गई।
जस्टिस चंद्रचूड़ की मीडिया में चर्चा
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे कहते हैं कि ‘मीडिया में उनका ज़बरदस्त प्रभाव रहा है।’
उनकी लोकप्रियता की वजह से ऑनलाइन ट्रोल्स ने भी जस्टिस चंद्रचूड़ को ख़ूब निशाना बनाया। उन्हें ‘हिंदू विरोधी’ और च्नक़ली महिलावादी’ कऱार दिया गया।
हालांकि, बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी जज को इतना ज़्यादा सुर्खय़िों में रहना चाहिए?
क्योंकि जज को तो समाज से अलग-थलग रहते हुए, मौजूदा बहाव से दूर रहकर केवल न्यायसंगत फ़ैसला करना चाहिए।
दुष्यंत दवे सवाल उठाते हैं, ‘आप मीडिया से इतना घुल-मिल रहे हैं तो आप ऐसे काम करना चाहेंगे जिससे लोग आपको पसंद करें फिर आप सख़्त फ़ैसले नहीं कर पाएँगे।’
मीडिया से बातचीत में जस्टिस चंद्रचूड़ ने हिंदू पहचान को खुलकर सामने रखा।
जनवरी में जब वो गुजरात के द्वारका मंदिर गए थे, तब जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि ‘मंदिर का ध्वज हम सबको एकजुट रखता है। उन्होंने मंदिर के ध्वज की तुलना संविधान से भी की थी।’
इसी साल गणेश चतुर्थी के पर्व के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, गणपति की पूजा के लिए उनके घर गए थे। इस बात की तीखी आलोचना की गई थी।
अक्टूबर महीने में लोगों को संबोधित करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान समाधान निकालने के लिए उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की थी।
इन सबकी आलोचना की गई और ये भी चंद्रचूड़ की विरासत का हिस्सा होगा।
सत्ता के शीर्ष और न्यायपालिका के प्रमुख के बीच निकटता दिखना एक जटिल बात है, अदालतों में सरकार ही सबसे ज़्यादा मामलों में पक्षकार होती है।
ऐसे में चीफ जस्टिस के रवैये से निचली अदालतों के लिए और जनता के बीच एक ख़ास तरह का संदेश जाता है।
अपना नाम ज़ाहिर न करने वाले सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश पूछते हैं, ‘आपको अपने घर में प्रधानमंत्री के साथ आरती करने की क्या ज़रूरत है? और अगर आप करते भी हैं, तो इसकी तस्वीरें जारी करने की क्या आवश्यकता थी?’
एक और पूर्व जज ने कहा कि ये कहना कि मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, ये बात आपको ‘अतार्किकता’ के मैदान में पहुंचा देती है और न्यायाधीशों को इससे बचना चाहिए।
यही नहीं, रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर ने कहा, ‘जज, सरकारी पदाधिकारियों से मिलते हैं लेकिन वो अक्सर सरकारी कार्यक्रमों में मिलते हैं। साथ में पूजा करने के लिए कभी नहीं मिलते।’
एक पूर्व न्यायाधीश कहते हैं, ‘वो बहुत मीठे हो सकते हैं। वो बहुत विनम्र हो सकते हैं, इसके बावजूद वो इतने आत्ममुग्ध रह सकते हैं कि दूसरों को नुक़सान पहुंचे।’
उन्होंने ये भी कहा कि ‘हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक नई इमारत के निर्माण की आधारशिला रखने का कार्यक्रम हुआ था लेकिन जब उसकी योजना भी नहीं तैयार है, तो फिर इसको करने की क्या ज़रूरत थी।’
चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के लोगो में भी बदलाव किया और न्याय की एक नई देवी की मूर्ति लगाई, जहां आंखों पर पड़ी पट्टी हटा दी गई है और न्याय की देवी के हाथ में संविधान है।
चीफ जस्टिस के तौर पर चंद्रचूड़ के कामकाज को लेकर वकीलों के संगठन ने भी कई शिकायतें कीं।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को चि_ी लिखकर शिकायत की कि उन्होंने ‘बार एसोसिएशन से सलाह-मशविरा किए बग़ैर ही सुप्रीम कोर्ट का प्रतीक चिह्न बदलने, न्याय की देवी का स्वरूप बदलने का फैसला ले लिया।’
ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने भी चीफ जस्टिस को चि_ी लिखी और आरोप लगाया कि वो वकीलों के सम्मान की हिफ़ाज़त कर पाने में नाकाम रहे हैं।
इसके साथ साथ उस चि_ी में ये भी कहा गया था कि चंद्रचूड़ का ‘बेशक़ीमती वक़्त कार्यक्रमों में जाने में बीत रहा है और अगर वो अपना व्यवहार नहीं बदलते हैं तो बार एसोसिएशन ये कहेगी कि चीफ जस्टिस अपने ओहदे की जि़म्मेदारियां निभाने से ज़्यादा ‘पब्लिसिटी’ पाने पर ज़ोर दे रहे हैं।’
फ़ैसले जो चर्चा में रहे
एक जज और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भी जस्टिस चंद्रचूड़ ऐसे कई अहम फ़ैसलों का हिस्सा थे, जिसने उन बुनियादी सिद्धांतों की नींव रखी, जो आने वाले समय में काफ़ी अहम साबित होने वाले हैं।
सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा, ‘आने वाले लंबे समय तक लोग उनके फ़ैसलों का असर महसूस करते रहेंगे।’ भारत में निजता के अधिकार को लेकर, उन्होंने 9 जजों की बेंच का बहुमत वाला फ़ैसला लिखा था।
इसका देश के सार्वजनिक जीवन के कई पहलुओं पर गहरा असर पडऩे वाला है। वो उन संविधान पीठों के सदस्य थे, जिसने समलैंगिकता और विवाहेत्तर संबंधों को अपराध बनाने के प्रावधान ख़त्म किए।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला भी लिखा था, जिसने अविवाहित महिलाओं को गर्भपात कराने का अधिकार दिया और सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की इजाज़त दी।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने 9 जजों की बेंच वाली एक और संवैधानिक बेंच के बहुमत वाले फ़ैसले को लिखा था, जिसमें कहा गया है कि सरकार के पास इस बात का अधिकार नहीं है कि वो किसी भी निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन मान ले और उसका पुनर्वितरण करे।
ऐसा करते हुए अदालत ने पिछले कई दशकों से चले आ रहे न्यायिक रुख़ से आगे बढऩे वाला क़दम उठाया, जिसमें कहा गया था कि सभी निजी संपत्तियां सामुदायिक संसाधन हैं।
अपने फ़ैसलों से जस्टिस चंद्रचूड़ ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण में उप-वर्ग बनाने की इजाज़त दी। जेलों में जाति पर आधारित भेदभाव को असंवैधानिक कऱार दिया। असम समझौतों की संवैधानिकता पर मुहर लगाई।
उत्तर प्रदेश में मदरसे चलाना जारी रखने की इजाज़त दी और 57 साल पुराने सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर सकती है।
जस्टिस चंद्रचूड़ ऐसे कई मुक़दमों की सुनवाई में शामिल थे, जो टैक्स लगाने और आर्बिट्रेशन से विवादों के निपटारे से जुड़े थे।
उनके कई फ़ैसलों में मीडिया और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ज़ोर देने की कोशिश दिखी। उन्होंने मलयालम के समाचार चैनल मीडिया वन के प्रसारण पर लगी पाबंदी को हटा दिया।
केंद्र सरकार की फ़ैक्ट चेक इकाई पर रोक लगा दी। वहीं, उन्होंने अर्नब गोस्वामी और ज़ुबैर अहमद को ज़मानत भी दी।
हालांकि, जस्टिस चंद्रचूड़ के बहुत से फ़ैसलों में ऐसा भी हुआ कि जो बुनियादी सिद्धांत तय किए गए, वो आने वाली पीढिय़ों के तो काम आएंगे।
लेकिन क़ानून के बहुत से जानकार ये सवाल उठाते हैं कि आखऱि वो कौन से फ़ायदे हैं, जो उनके इन फ़ैसलों से निकलेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज ने कहा, ‘उनके बहुत से फ़ैसलों की ये ख़ूबी रही है। उनके अंदर इस बात की क़ाबिलियत है कि वो ऐसे सिद्धांतों को तलाश करके उनको आधार बना दें, जो आने वाली पीढिय़ों के काम आएं। ये सब तो ठीक है। लेकिन, ये सवाल भी उठता है कि आखऱि में अदालत ने किया क्या?’
इन पूर्व न्यायाधीश ने ये भी कहा, ‘मुझे लगता है कि वो चोट करने के लिए तो तैयार थे, मगर किसी को घायल करने से डरते थे, जो एक परेशान करने वाली बात है।’
मिसाल के तौर पर उनका एक फ़ैसला इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर था, जिसकी सराहना की गई थी।
उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को रद्द कर दिया और सरकार पर इसके आंकड़े जारी करने का दबाव बनाया, ताकि दान देने वालों के नाम राजनीतिक दलों को मिले चंदे से मिलाए जा सकें।
हालांकि, इसके बाद अदालत ने कोई कार्रवाई करने से परहेज़ किया। लेन-देन के कई मामले सामने आए, जांच एजेंसियों की छापेमारी के बाद इलेक्टोरल बॉण्ड से चंदे दिए गए,
या फिर बॉण्ड से चंदा दिए जाने के बाद सरकारी ठेके मिले। लेकिन अदालत ने ऐसे मामलों पर कोई कार्रवाई करने से साफ़ इनकार कर दिया।
इस मामले में अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिका दायर करने वाले संगठन के वकील प्रशांत भूषण थे। इस मामले की सुनवाई चार महीने बाद के लिए निर्धारित की गई और एक ही सुनवाई के बाद याचिका को ख़ारिज कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज ने कहा, ‘इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने के बाद जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उसमें बहुत कमियां रह गईं।’
दुष्यंत दवे कहते हैं, ‘ये मामला ऐसा था कि ऑपरेशन कामयाब रहा पर मरीज़ मर गया।’
ऐसे कई मामले रहे जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने उनको अहम समझते हुए उनका ख़ुद से संज्ञान लिया और अदालत की निगरानी में जांच का आदेश दिया।
उन्होंने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में रेप और हत्या और मणिपुर के यौन हिंसा मामले की सुनवाई ख़ुद संज्ञान लेकर की। उन्होंने मणिपुर हिंसा मामले की विशेष जांच टीम से तफ़्तीश का आदेश भी दिया।
लेकिन इस बारे में कोई साफ़ पैटर्न नहीं दिखा कि वो किस तरह के मामलों का ख़ुद से संज्ञान लेंगे या फिर अदालत की निगरानी में किस तरह के मामलों की जांच का आदेश देंगे।
मसलन, उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करने वाली कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से अडानी समूह की कंपनियों पर लगाए गए आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच का आदेश देने से मना कर दिया।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फ़ैसले में कहा कि सेबी की जांच पर ‘भरोसा पैदा होता है’ और ऐसे मामलों की जांच सेबी से लेकर किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है।
हालांकि, इसकी आलोचना की गई क्योंकि सेबी की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे थे।
इसी तरह का मामला, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 39 विधायकों का टूटकर एकनाथ शिंदे गुट में जाने का था जिसकी वजह से जून 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी।
वैसे तो अदालत ने इस मामले की सुनवाई उस वक़्त शुरू की, जब चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस नहीं बने थे। लेकिन मामले का फ़ैसला चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस बनने के छह महीने के भीतर हो गया था।
वैसे तो फ़ैसला आखऱि में उद्धव ठाकरे के पक्ष में गया लेकिन इसमें अदालत ने कहा कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया है, इसलिए अदालत कुछ नहीं कर सकती।
सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश कहते हैं, ‘महाराष्ट्र में इस बात की जीती-जागती मिसाल थी कि सरकार काम कर रही थी। ऐसे में वो (उद्धव ठाकरे को दोबारा मुख्यमंत्री पद पर बहाल करके) इतिहास क़ायम कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं किया।’
चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के मामले में इसके ठीक उलट हुआ, जहां अदालत ने मामले की तेज़ी से सुनवाई की और चुनाव के नतीजों को पलट दिया।
इसी तरह जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये फ़ैसला भी दिया कि दिल्ली की सिविल सेवाओं पर उप-राज्यपाल का नहीं, दिल्ली की चुनी हुई सरकार का नियंत्रण होगा।
हालांकि उनके इस फ़ैसले को पलटने के लिए सरकार दस दिनों बाद ही एक अध्यादेश ले आई, जिसे बाद में क़ानून में तब्दील किया गया। इस क़ानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई मगर चंद्रचूड़ के पूरे कार्यकाल में ये मामला लंबित ही रहा।
जब जस्टिस चंद्रचूड़ जज थे, तो उन्हें आमतौर पर गर्भपात के समर्थक के तौर पर देखा जाता था क्योंकि 2022 में उन्होंने फ़ैसला दिया था कि अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात का अधिकार होना चाहिए।
अपने फ़ैसले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था, ‘केवल महिला को ही अपने शरीर पर अख़्तियार है, और गर्भपात की तमाम वजहें हो सकती हैं, इनमें मानसिक सेहत भी शामिल है।’
हालांकि 2023 में उन्होंने एक और बहुचर्चित फ़ैसला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक शादीशुदा महिला को गर्भपात कराने की इजाज़त दी, जो 26 हफ़्ते की गर्भवती थी।
लेकिन आखऱि में जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने गर्भपात की इजाज़त देने से इ3कार कर दिया।
महिला ने कहा कि वो भयंकर मानसिक और शारीरिक चुनौतियों से जूझ रही है और उसको अपने गर्भवती होने की ख़बर बहुत देर से हुई, और इसी वजह से वो पहले अदालत नहीं आ सकी थी।
फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उस महिला को गर्भपात की इजाज़त नहीं दी कि इससे ‘गर्भ में पल रहे बच्चे के जीने के अधिकार का हनन’ होगा।
आलोचकों ने इस मामले को भारत में गर्भपात के अधिकारों के संदर्भ में उल्टी दिशा में जाने वाला फ़ैसला करार दिया था, जिसने अपने शरीर पर महिला के अधिकार को कमज़ोर बना दिया।
जब बात फेडरलिज्म की आई तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने खनिजों के उत्खनन और औद्योगिक एल्कोहल पर टैक्स लगाने के राज्यों के अधिकार पर मुहर लगाई।
मगर अनुच्छेद 370 के मामले में उन्होंने इसे हटाने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने को जायज़ ठहराया।
ऐसा फ़ैसला देते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस सवाल से किनारा कर लिया कि क्या केंद्र किसी राज्य को बांट सकता है और वो भी राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत, जब राज्य की अपनी विधानसभा काम न कर रही हो।
उनके इस फ़ैसले की आलोचना हुई थी और इसे संघवाद को कमज़ोर करने वाले फ़ैसले के तौर पर देखा गया था।
अयोध्या मामले में भी जस्टिस चंद्रचूड़ की भूमिका के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। चंद्रचूड़ उस बेंच में शामिल थे, जिसने वो फ़ैसला सुनाया था, जिस पर कई सवाल उठाए गए थे।
अपने फ़ैसले में अदालत ने मस्जिद ढहाने को ग़ैरक़ानूनी माना था और ये भी स्वीकार किया था कि पुरातात्विक सर्वेक्षण में ये साबित नहीं हुआ है कि बाबरी मस्जिद को किसी मंदिर को तोडक़र बनाया गया था, फिर भी अदालत ने विवादित ज़मीन हिंदुओं को दे दी और मुसलमानों को एक और मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ ज़मीन दूसरी जगह आवंटित करने का आदेश दे दिया।
इस फ़ैसले का हैरान करने वाला एक पहलू ये भी था कि फ़ैसला लिखने वाले जज के नाम का जि़क्र नहीं था, जो एक अजीब बात है।
बाद में पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में चंद्रचूड़ ने कहा कि ये ऐसा फ़ैसला था, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच ने तय किया था कि इसको लिखने वाले जज का नाम नहीं होना चाहिए। पर चूंकि, सुप्रीम कोर्ट जो भी फ़ैसला देता है, वो कोई भी बेंच दे, उसे सर्वोच्च न्यायालय का ही फ़ैसला कहा जाता है।
हालाँकि रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद वाले फ़ैसले में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रावधानों पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है।
ये क़ानून अयोध्या विवाद के बाद बनाया गया था ताकि आज़ादी के वक़्त किसी धार्मिक स्थल की जो स्थिति रही थी, उसे ही बरकऱार रखा जाए।
इस क़ानून में किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदलने पर भी पाबंदी लगाई गई है। बहुत से लोगों को लगा था कि इससे भविष्य में मंदिर-मस्जिद का कोई और विवाद खड़ा होने से रोका जा सकेगा।
हालांकि जब ज्ञानवापी मंदिर का विवाद जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने सुनवाई के लिए आया, तो उन्होंने इससे जुड़े मामलों को चलने दिया।
उन्होंने ये कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की जांच के लिए सर्वे कराने पर रोक नहीं लगाता कि आज़ादी के वक़्त किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप क्या था।
आज भी ज्ञानवापी का विवाद और ऐसे ही कई मामले अदालतों में विचाराधीन हैं।
वैसे तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने निजता के अधिकार से जुड़ा फ़ैसला भी लिखा और आधार के मामले में बहुमत से अलग वो फ़ैसला भी लिखा था, जिसकी कुछ लोग बहुत तारीफ़ करते हैं।
उस फ़ैसले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि 12 अंकों वाले जिस पहचान पत्र को सरकार ले आई है, वो ‘असंवैधानिक’ है और इसे ख़त्म कर दिया जाना चाहिए।
लेकिन इसके बरअक्स सरकार के आलोचकों की जासूसी के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के मामले भी उनके कार्यकाल में लंबित रहे। इसकी एक बार भी सुनवाई नहीं हुई।
आधार के अलावा, जस्टिस चंद्रचूड़ को कई और मामलों में भी बहुमत से अलग फ़ैसला देने के लिए याद किया जाता है।
जैसे कि भीमा कोरेगांव का मामला, इसमें बहुमत से अलग फ़ैसला सुनाते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस का रवैया उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है और भीमा कोरेगांव के मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में फिर से जांच होनी चाहिए।
हालांकि चंद्रचूड़ का कार्यकाल ख़त्म होने तक भी भीमा कोरेगांव से जुड़े मामलों में ट्रायल शुरू नहीं हो सका है। जबकि, उनके चीफ जस्टिस रहते हुए (दूसरी बेंचों ने) इस मामले में गिरफ़्तार कम से कम तीन लोगों को ज़मानत ज़रूर दे दी है।
लेकिन, इसकी तुलना में एक जि़ला जज बीएच लोया की मौत के केस में जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसकी स्वतंत्र रूप से जांच की मांग करने वाली तमाम याचिकाओं को ख़ारिज करने वाला फ़ैसला सुनाया था।
मौत के वक़्त जज लोया, सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मुख्य आरोपी थे।
इस मामले की सुनवाई जिस तरह हुई और उसके बाद चंद्रचूड़ के इस फ़ैसले की व्यापक रूप से आलोचना हुई थी। इसकी लिस्टिंग और अदालतों में सुनवाई के दौरान दिए गए तर्कों पर सवाल उठाए गए थे।
क़ानूनी मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार मनु सैबेस्टियन ने फ़ैसले की तुलना करते हुए इसे आज के दौर का ‘एडीएम जबलपुर केस’ बताया था।
एडीएम जबलपुर केस की बहुत आलोचना की जाती है। आपातकाल के दौरान आम लोगों के अधिकारों को निलंबित करने वाले इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता भी शामिल रहे थे जिसने अधिकारों के निलंबन को सही ठहराया था।
तकनीकी सुधार
एक पहलू जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई बदलाव लाए वो अदालतों के आधुनिकीकरण का है। सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति के अध्यक्ष के तौर पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई क़दम उठाए।
अब संविधान पीठ की सुनवाई की ट्रांसक्रिप्ट उपलब्ध हैं। आर्टिफि़शियल इंटेलिजेंस की मदद से फ़ैसलों का सभी भाषाओं में अनुवाद किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट सभी अदालतों की सुनवाई के लाइव प्रसारण की तैयारी कर रहा है।
सीनियर वकील संजय हेगड़े ने कहा, ‘अदालत के आधुनिकीकरण में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वीडियो कांफ्रेंस की व्यवस्था को बेहतर बनाया। ई-फाइलिंग की स्वीकार्यता बढ़ाई। वो सुप्रीम कोर्ट को आधुनिक बनाने और सरकार से फंडिंग हासिल करने की एक अच्छी विरासत छोडक़र जा रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बारीक़ी से सार्वजनिक पड़ताल करने के दरवाज़े भी खोले हैं।’
जस्टिस चंद्रचूड़ की विरासत
वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे कहते हैं, ‘उनका कार्यकाल तबाही लाने वाला रहा है और वो अपने पीछे बहुत से लोगों को नाख़ुश करने वाली खऱाब विरासत छोडक़र जा रहे हैं।’
वैसे बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि चंद्रचूड़ का कार्यकाल मिला-जुला रहा है।
संजय हेगड़े कहते हैं, ‘जहां तक तकनीकी सुधार और जनता की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच की बात है, तो उन्होंने ज़ाहिर तौर पर इसे बेहतर बनाया है। लेकिन, जब बात नैतिकता वाले प्रभुत्व की आती है, तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत आगे नहीं बढ़ सका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के प्रभाव में कितनी गिरावट आई है और इसकी छवि को कितना नुक़सान पहुंचा है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल सकेगा।’
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर कहते हैं, ‘कुछ संदेहास्पद फ़ैसलों के बावजूद न्यायिक पहलू के मामले में उनका कार्यकाल अच्छा रहा है। और जहां तक प्रशासनिक पहलू की बात है, तो ये और बेहतर हो सकता था।’
जाने-माने वकील प्रशांत भूषण को लगता है, ‘चंद्रचूड़ को ये अदालत जिन हालात में मिली थी, वो इसे और बेहतर स्थिति में छोडक़र नहीं जा रहे हैं। हम सबको जस्टिस चंद्रचूड़ से बहुत उम्मीदें थीं। (bbc.com/hindi)