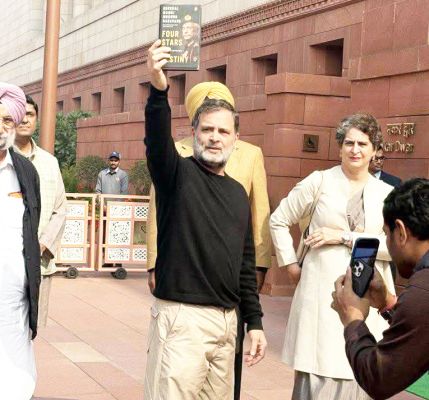विचार / लेख

-अमिताभ पाराशर
दाई सीरो देवी रोते हुए मोनिका थट्टे से लिपट गईं। 30 की उम्र के करीब पहुंच रहीं मोनिका उस जगह लौटी हैं, जहां वो पैदा हुई थीं।
उस भारतीय शहर में, जहां सीरो देवी ने सैकड़ों बच्चे पैदा करवाए थे। लेकिन ये कोई सहज पुनर्मिलन नहीं था। सीरो के आंसुओं के पीछे दर्द भरा इतिहास है।
मोनिका के जन्म के कुछ समय पहले तक सीरो देवी और उनकी जैसी कई दाइयों पर इस बात का लगातार दबाव रहता था कि वो नवजात बच्चियों को मार डालें।
सबूत बताते हैं कि मोनिका उन बच्चियों में शामिल थीं, जिन्हें उन्होंने बचाया था।
मैं सीरो देवी की कहानी को पिछले 30 सालों से फॉलो कर रहा हूं। ये 1996 की बात है जब मैंने बिहार जाकर सीरो देवी और उनकी जैसी ग्रामीण इलाकों में काम करने वाली चार और दाइयों का इंटरव्यू किया था।
एक एनजीओ ने इस बात का पता लगाया था कि बिहार के कटिहार जि़ले में नवजात बच्चियों की मौत में इन दाइयों का हाथ था। ये दाइयां माता-पिता के दबाव में आकर उनकी नवजात बच्चियों की हत्या कर रही थीं।
अमूमन उन्हें केमिकल चटा कर या फिर उनकी गर्दन मरोड़ कर मारा जा रहा था।
मैंने जिन दाइयों का इंटरव्यू किया था, उनमें सबसे उम्रदराज़ थीं हकिया देवी। उन्होंने मुझे उस समय बताया था कि उन्होंने 12-13 बच्चियों को मार दिया था।
एक और दाई धरमी देवी ने यह स्वीकार किया था कि उन्होंने इससे ज़्यादा यानी कम से कम 15-20 बच्चियों को मारा है।
हालांकि जिस तरह से आंकड़े जुटाए गए थे, उससे ये बताना मुश्किल है कि आखिर ऐसी कितनी बच्चियों को मारा गया होगा।
मगर 1995 में एक एनजीओ की रिपोर्ट में उनकी और उनकी जैसी 30 दाइयों के इंटरव्यू के आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। अगर इस रिपोर्ट का आकलन सटीक माना जाए तो सिर्फ 35 दाइयां ही हर साल एक जिले में एक हजार से अधिक बच्चियों को मार रही थीं।
उस रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार में उस समय 5 लाख से ज़्यादा दाइयां काम करती थीं और शिशु हत्या सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं थी।
हकिया देवी ने बताया था किसी भी दाई के लिए नवजात बच्ची को मार देने का आदेश मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। (बाकी पेज 8 पर)
हकिया देवी ने बताया, ‘परिवार कमरा बंद कर हमारे पीछे डंडे लेकर खड़ा हो जाता था। फिर वो कहते हमारी पहले से चार-पांच बेटियां हैं। हमारी सारी जमा-पूंजी इन्हीं पर खत्म हो जाएगी। चार लड़कियों को दहेज देने के बाद हमारे सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। अब एक और लडक़ी पैदा हो गई है। मार दो इसे।’
उन्होंने मुझे बताया, ‘हम किससे शिकायत करते? हमें डर था। अगर हम पुलिस के पास जाते तो फँस जाते। और अगर हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते तो हमें गांव के लोग धमकाते।’
वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ पाराशर 1990 के दशक में दाइयों से किए गए उस असाधारण इंटरव्यूज को देखते हुए। कमरे में अंधेरा था और उनके चेहरे पर स्क्रीन की रोशनी थी।
इमेज कैप्शन,अमिताभ 1990 के दशक में दाइयों से किए गए उन असाधारण इंटरव्यूज़ को देखते हुए।
ग्रामीण भारत में दाइयों की भूमिका परंपरा की जड़ में है। ये गरीबी और जाति की कठोर सच्चाइयों के बोझ से दबी है। मैंने जिन दाइयों के इंटरव्यू किए वो भारत की जाति व्यवस्था में निचली जातियों से आती हैं।
ये दाइयां बच्चे पैदा करवाने का ये काम अपनी मां और दादी-नानी से सीखती थीं। वे एक ऐसी दुनिया में रहती थीं, जहां ताक़तवर और ऊंची जाति के परिवारों के आदेश का पालन न करने की बात सोची भी नहीं जा सकती थी।
एक दाई को किसी बच्ची को मारने के एवज में एक साड़ी, एक बोरी अनाज या फिर कुछ पैसे देने का वादा किया जाता था। लेकिन कभी-कभी ये भी नहीं मिलता था। लडक़ा पैदा होने पर एक हजार रुपये दिए जाते थे, जबकि लडक़ी पैदा होने पर 500 रुपये।
उन्होंने बताया कि इस असंतुलन की जड़ें भारत में दहेज लेने-देने की परंपरा में है। हालांकि दहेज लेन-देन की प्रथा को 1961 में गैर-क़ानूनी बना दिया गया।
मगर 1990 के दशक में भी दहेज लेने-देने की प्रथा मजबूत बनी हुई थी और आज भी ये बदस्तूर जारी है।
दहेज के तौर पर कुछ भी हो सकता है। जैसे- नकदी, गहने, बर्तन वगैरह। लेकिन कई परिवारों के लिए चाहे वो अमीर हो या गऱीब, दहेज शादी की शर्त होती है।
यही वो वजह है कि कइयों के लिए आज भी बेटे का जन्म उत्सव है और बेटी का जन्म एक आर्थिक बोझ।
जिन दाइयों का मैंने इंटरव्यू किया, उनमें सीरो देवी अभी भी जीवित हैं। उन्होंने लडक़ी और लडक़े के बीच इस असमानता को समझाने के लिए एक उदाहरण का सहारा लिया।
उन्होंने कहा, ‘लडक़े का दर्जा ऊपर है। लडक़ी का नीचा। बेटा भले ही अपने मां-बाप का ख़्याल न रखे लेकिन सब बेटा ही चाहते हैं।’
भारत में राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों में बेटे को दी जाने वाली तवज्जो दिख सकती है।
सबसे हालिया, 2011 की जनगणना में देश में प्रति 1000 पुरुषों में 943 महिलाओं का अनुपात था।
1990 के दशक यानी 1991 की जनगणना के मुकाबले यह फिर भी ठीक था। तब यह अनुपात एक हजार पुरुषों के मुकाबले 927 महिलाओं का था।
1996 तक जब मैंने इन दाइयों के सबूतों को फिल्माना ख़त्म किया, तब तक एक मौन बदलाव शुरू हो गया था। पहले बच्चियों को मारने का आदेश चुपचाप सुन लेने वाली दाइयों ने अब इसका प्रतिरोध करना शुरू कर दिया था।
इस बदलाव के लिए उन्हें अनिला कुमारी ने प्रेरित किया था। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं, जो उन दिनों कटिहार के आसपास की महिलाओं की मदद कर रही थीं। अनिला कुमारी नवजात बच्चियों की हत्या की असल वजहों को ख़त्म करने के लिए समर्पित थीं।
अनिला का तरीका आसान था। वो इन दाइयों से पूछतीं- क्या तुम अपनी बेटी के साथ भी यही करती?
सालों से जिन चीज़ों को स्वीकार कर लिया गया था, इस सवाल से उस सोच को झटका लगा।
इन दाइयों को सामुदायिक समूहों के जरिए कुछ वित्तीय मदद मिली। फिर धीरे-धीरे हिंसा का ये चक्र बाधित हो गया था।
सीरो देवी ने 2007 में बात करते हुए मुझे इस बदलाव के बारे में समझाया था।
उन्होंने बताया था, ‘अब कोई मुझसे बच्ची को मारने को कहता है तो मैं उनको कहती हूं कि देखो, बच्ची मुझे दे दो। मैं उसको अनिला मैडम के पास ले जाऊंगी।’
उन दाइयों ने उन परिवारों के कम से पांच नवजात बच्चियों को बचाया था जो या तो उन्हें मरवाना चाहते थे या फिर उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था।
एक बच्ची तो बच नहीं पाई। लेकिन अनिला ने चार बच्चियों को पटना के एक एनजीओ को भिजवा दिया। वहां उस एनजीओ ने उन बच्चियों को गोद देने की व्यवस्था कर दी।
यह कहानी यहीं खत्म हो सकती थी। मगर, मैं जानना चाहता था कि उन बच्चियों का क्या हुआ, जिन्हें बचा कर गोद दे दिया गया था। जिंदगी उनको कहां ले कर चली गई थी।
अनिला के रिकॉर्ड बड़ी ही सावधानी और तफसील से बने थे। लेकिन गोद दिए गए बच्चों की बाद की जिंदगी के बारे के बारे में ब्योरे कम थे।
बाद में मेरा परिचय मेधा शेखर नाम की एक महिला से हुआ। वो नब्बे के दशक में बिहार में भ्रूण हत्या पर रिसर्च कर रही थीं। ये वही वक्त था जब अनिला और दाइयों की बचाई गई बच्चियां एनजीओ पहुंचाई जा रही थीं।
आश्चर्यजनक रूप से मेधा अभी भी एक युवा महिला के संपर्क में थीं, जिनके बारे में उन्हें विश्वास था कि वो उन बचाई गई बच्चियों में से एक हैं।
अनिला ने मुझे बताया कि दाइयों की ओर से बचाई गई सभी बच्चियों को नाम दिए जाने से पहले ही उन्होंने उनके नाम के आगे कोसी जोड़ दिया था। ये बिहार की नदी कोसी को दी गई उनकी श्रद्धांजलि थी।
मेधा को याद है कि मोनिका के नाम के आगे भी ‘कोसी’ उपनाम जोड़ा गया था। यह उसको गोद लिए जाने से पहले की बात है।
गोद देने वाली एजेंसी हमें मोनिका के रिकॉर्ड नहीं देखने देती। लिहाजा हमारे पास उनकी असली पहचान जानने को कोई ज़रिया नहीं हो सकता था।
लेकिन उनके मूल स्थान पटना, उनकी जन्मतिथि की नजदीक की तारीखों और नाम से पहले ‘कोसी’ का जुड़ा होना- हमें उसी समान निष्कर्ष की ओर से ले गया। और वो ये कि वो संभवत: उन पांच बच्चियों में से एक हैं जिसे अनिला और दाइयों ने बचाया था।
जब मैं उनसे (मोनिका) मिलने 2000 किलोमीटर दूर पुणे पहुंचा था तो उन्होंने कहा था कि वो खुशकिस्मत हैं कि एक प्यारे परिवार ने उन्हें गोद लिया।
लाल और सफेद कुर्ते में बैठी मोनिका अपने पिता की ओर झुकी हुईं। क्रीम रंग की शर्ट पहने इसी शख़्स ने उन्हें गोद लिया था।
उन्होंने कहा, ‘एक सामान्य खुशहाल जिंदगी की मेरी परिभाषा यही है और मैं ये जि़ंदगी जी रही हूं।’
मोनिका जानती थीं कि उन्हें बिहार से गोद लिया गया था। लेकिन हम मोनिका को उन्हें गोद दिए जाने की परिस्थितियों के बारे में ज्यादा ब्योरे दे पाए थे।
इस साल की शुरुआत में मोनिका ने अनिला और सीरो देवी से मुलाकात करने के लिए बिहार की यात्रा की।
मोनिका ख़ुद को अनिला और उन दाइयों जैसी महिलाओं के कठिन परिश्रम की परिणति के तौर पर देख रही थीं।
मोनिका ने कहा, ‘इम्तिहान में अच्छा करने के लिए जैसे कोई काफी तैयारी करता है, मैं वैसा ही महसूस कर रही थी। उन्होंने कड़ी मेहनत की थी और नतीज़ा देखने के लिए इतनी उत्सुक थीं। निश्चित तौर पर मैं उन लोगों से मिलना चाहती थी।’
मोनिका से मिलने के वक्त अनिला की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन सीरो की प्रतिक्रिया कुछ अलग तरह की थी।
उन्होंने मोनिका को गले लगाया और जोर-जोर से सुबकने लगीं। वो मोनिका के बालों में कंघी करने लगीं।
उन्होंने कहा, ‘तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मैं तुम्हें एक अनाथालय ले गई थीज् अब मेरी आत्मा को शांति मिली है।’ लेकिन ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी कुछ लोगों के मन में बच्चियों के लिए पूर्वाग्रह है।
शिशु हत्या की ख़बरें तुलनात्मक तौर पर अब दुर्लभ हैं। लेकिन लिंग के आधार पर भ्रूण हत्या के मामले अब भी देखने को मिल जाते हैं, इसके बावजूद कि सरकार ने 1994 में ही इसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया था
उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बच्चों के जन्म के समय गाए जाने वाले लोक गीत सोहर को कोई सुने तो पता चलेगा जन्म की खुशियां सिफऱ् लडक़ों के लिए सुरक्षित रखी गई हैं।
साल 2024 में भी स्थानीय गायकों को गानों के बोल बदलवाने की कोशिश करनी पड़ती है ताकि बच्चियों के पैदा होने की खुशी झलके।
जब हम अपनी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग कर रहे थे, तब कटिहार में दो नवजात बच्चियां मिली थीं।
इनमें से एक बच्ची को झाडिय़ों में जबकि दूसरी को सडक़ किनारे छोड़ दिया गया था। दोनों बच्चियों को जन्म लिए कुछ घंटे हुए थे। बाद में उनमें से एक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरी को गोद लिए जाने के लिए भेज दिया गया था।
मोनिका ने बिहार छोडऩे से पहले कटिहार के स्पेशल अडॉप्शन सेंटर में इस बच्ची को जाकर देखा।
उसने बताया कि वह इस अहसास से ही डर गई थीं कि शिशु हत्या भले ही कम हो गई हो लेकिन अभी भी बच्चियों को जन्म के बाद छोड़ दिया जाना जारी है।
‘यह एक चक्र है। मैं देख सकती हूं कि कुछ साल पहले मैं जिस जगह थी, आज कोई और लडक़ी मेरी जैसी स्थिति में है।’
मगर, कुछ ऐसी समानताएं भी थीं, जिन्हें लेकर खुश हुआ जा सकता है।
उस बच्ची को उत्तर-पूर्वी राज्य असम के एक दंपति ने गोद लिया था। उन्होंने उसे ईधा नाम दिया था। जिसका मतलब है खुशी।
उसे गोद लेने वाले पिता गौरव ने बताया, '' हमने उसकी फोटो देखी और हमने तय कर लिया कि एक बच्ची को एक बार छोड़ दिया गया। उसे दूसरी बार नहीं छोड़ा जा सकता है।''
गौरव भारतीय वायु सेना में एक अधिकारी हैं।
हर कुछ हफ्तों में गौरव मुझे उस बच्ची का नया वीडियो भेजते हैं। कुछ मौकों पर मैं उन वीडियो को मोनिका के साथ भी साझा करता हूं।
पीछे मुडक़र देखता हूं तो लगता है कि इस कहानी पर 30 साल खर्च करना सिर्फ अतीत का आख्यान नहीं है।
ये परेशान करने वाली सच्चाइयों से रूबरू होना था। अतीत की गलतियों को मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन अब बदलाव संभव है। इस बदलाव में ही उम्मीद है। (www.bbc.com/hindi)