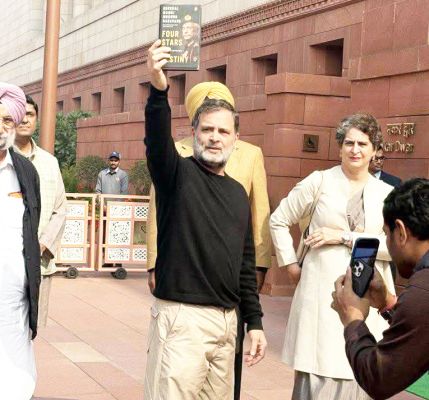विचार / लेख
-नवीन सिंह खडक़ा
हाल के हफ़्तों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण भारत के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। इस कारण कई लोगों की जान गई है और हज़ारों विस्थापित हुए हैं।
साल के इन महीनों में जब सबसे अधिक बारिश होती है, भारत या दक्षिण एशिया में बाढ़ आना कोई असामान्य बात नहीं है।
लेकिन जलवायु परिवर्तन ने मॉनसून की बारिश को अधिक अनियमित बना दिया है, मसलन लंबे समय समय तक सूखा रहने के बाद किसी जगह पर अचानक बहुत कम समय में मूसलाधार बारिश हो जाना।
अब वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण नमी में बहुत अधिक वृद्धि के साथ एक किस्म का तूफ़ान हालात को और बिगाड़ रहा है। इस तूफ़ान को ‘एटमॉस्फ़ेरिक रिवर’ या ‘वायुमंडलीय नदी’ के नाम से जाना जाता है।
आसमान में बनने वाले इन तूफ़ानों को ‘फ्लाइंग रिवर्स’ या ‘वायुमंडलीय नदियां’ भी कहते हैं। ये पानी के भाप वाले रिबन बैंड जैसे होते हैं जो गऱम समंदर से होने वाले वाष्पीकरण से बनते हैं और अदृश्य होते हैं।
ये भाप वायुमंडल के निचले हिस्से में एक पट्टी की तरह बनाते हैं जो उष्णकटिबंधीय इलाक़ों से ठंडे प्रदेशों की ओर बढ़ता है और बारिश या बर्फ के रूप में गिरता है।
यह किसी इलाके में बाढ़ या भयावह बर्फीला तूफान लाने के लिए पर्याप्त विनाशकारी होता है।
ये ‘फ्लाइंग रिवर्स’ कुल जल वाष्प का 90 फीसदी हिस्सा लेकर चलती हैं और पृथ्वी के मध्य-अक्षांश के ऊपर से होकर गुजरती हैं। औसतन इनमें अमेजन नदी में आम तौर पर बहने वाले पानी का दोगुना पानी होता है।
पानी की मात्रा के लिहाज़ से अमेजऩ नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है।
जितनी तेज़ी से पृथ्वी गर्म हो रही है, वैज्ञानिकों का कहना है कि ये ‘एटमास्फेरिक रीवर्स’ और बड़ी, चौड़ी और अधिक तीव्र होती जा रही हैं। इसकी वजह से पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों पर बाढ़ का जोखिम बढ़ गया है।
भारत में मौसम विज्ञानियों का कहना है कि हिंद महासागर के गर्म होने से ‘फ्लाइंग रिवर्स’ बन रही हैं जो जून और सितंबर के बीच इस क्षेत्र में होने वाली मॉनसून की बारिश पर असर डाल रही हैं।
भयावह होती जा रही ‘फ्लाइंग रिवर्स’
वैज्ञानिक पत्रिका ‘नेचर’ में 2023 में प्रकाशित एक अध्ययन दिखाता है कि 1951 से 2020 के बीच भारत में मॉनसून सीजन के दौरान कुल 574 ‘वायुमंडलीय नदियां’ बनीं। समय के साथ इनके बनने में तेजी आई है।
अध्ययन में कहा गया है, ‘पिछले दो दशकों में, कऱीब 80 फ़ीसदी सबसे ख़तरनाक ‘वायुमंडलीय नदियां’ भारत में बाढ़ का कारण बनीं।’
इस अध्ययन में शामिल आईआईटी और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की टीम ने यह भी पाया कि 1985 और 2020 के बीच मॉनसून के सीजऩ में भारत के 10 में से 7 सबसे भयावह बाढ़ों का कारण ये ‘वायुमंडलीय नदियां’ रही हैं।
अध्ययन में कहा गया है कि हाल के दशकों में हिंद महासागर में वाष्पीकरण की प्रक्रिया में ख़ासा इजाफ़ा हुआ है और इस तरह की ‘वायुमंडलीय नदियां’ बनने की प्रक्रिया तेज हुई है। और फिर ग्लोबल वार्मिंग के कारण हाल के दिनों में इसके कारण बाढ़ की घटनाएं भी बढ़ गई हैं।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ ट्रापिकल मेटीरियोलॉजी में एटमॉस्फ़ेरिक वैज्ञानिक डॉ.रॉक्सी मैथ्यू कोल ने बीबीसी को बताया, ‘मानसून सीजऩ के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बहने वाली नमी में उतार-चढ़ाव की घटनाएं बढ़ गई हैं।’
‘परिणामस्वरूप, गरम समंदर की कुल नमी को ‘फ्लाइंग रिवर्स’ कुछ घंटों या कुछ दिनों के अंदर ही छोड़ देती हैं। इसकी वजह से पूरे देश में भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ की संख्या बढ़ गई है।’
कैसी होती हैं ‘फ्लाइंग रिवर्स’?
एक ‘फ्लाइंग रिवर’ या ‘वायुमंडलीय नदी’ की औसत लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर और चौड़ाई 500 किलोमीटर तक होती है। इसकी गहराई तीन किलोमीटर तक हो सकती है। हालांकि अब ये और लंबी और चौड़ी होती जा रही हैं और कुछ की लंबाई 5,000 किलोमीटर से अधिक हो सकती है।
बावजूद इसके, ये इंसानी आंखों के लिए अदृश्य होती हैं।
नासा के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के साथ काम करने वाले एटमॉस्फेरिक रीसर्चर ब्रायन कान कहते हैं, ‘इन्हें इनफ्रारेड और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के द्वारा देखा जा सकता है।’
उनके मुताबिक, ‘यही कारण है कि पूरी दुनिया में भाप के बादलों और वायुमंडलीय नदियों की निगरानी के लिए सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन कारगर हो सकता है।’
इसके अलावा मौसम की कुछ और घटनाएं भी हैं जैसे पश्चिमी विक्षोभ, मानसून और चक्रवात, जो बाढ़ पैदा कर सकते हैं।
लेकिन वैश्विक अध्ययनों ने दिखाया है कि 1960 के दशक से ही वायुमंडल में भाप के बादलों में 20 फीसदी तक की वृद्धि हुई है।
वैज्ञानिकों ने दक्षिण एशिया में 56त्न तक अत्यधिक बारिश और बर्फबारी को वायुमंडलीय नदियों से जोड़ा है, हालांकि इस क्षेत्र में अभी सीमित अध्ययन हैं।
मानसून से जुड़ी भारी बारिश और वायुमंडलीय नदियों के बीच के संबंध को लेकर पड़ोसी दक्षिण पूर्व एशिया में अधिक विस्तृत अध्ययन हुए हैं।
अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन द्वारा प्रकाशित साल 2021 में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि पूर्वी चीन, कोरिया और पश्चिमी जापन में मानसून सीजऩ (मार्च और अप्रैल) के दौरान 80 फीसदी भारी बारिश की घटनाओं का संबंध वायुमंडलीय नदियों से जुड़ा है।
पोस्टडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रीसर्च से जुड़ी सारा एम वालेजो-बर्नाल का कहना है, ‘1940 से ही पूर्वी एशिया में वायुमंडलीय नदियां बनने की घटनाओं में ख़ासी वृद्धि हुई है।’
उनके अनुसार, ‘हमने पाया है कि उसके बाद से ही मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और जापान में ये बहुत तीव्र होती गई हैं।’
अन्य हिस्सों के मौसम वैज्ञानिकों ने हाल में हुई कुछ बड़ी बाढ़ की घटनाओं को वायुमंडलीय नदियों से जोड़ा है।
इराक, ईरान, कुवैत और जॉर्डन में भारी बारिश के पीछे वायुमंडलीय नदियां?
2023 के अप्रैल में इराक, ईरान, कुवैत और जॉर्डन को ओलावृष्टि, और भारी वर्षा के बाद प्रलयकारी भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ा था।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यहाँ के इन इलाकों में आसमान में नमी की रिकॉर्ड मात्रा थी जो 2005 के इसी तरह की घटना से भी ज्यादा थी।
ठीक दो महीने बाद चिली में महज तीन दिनों में 500 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई। इन तीन दिनों में इतनी बारिश हुई कि इसने एंडीज पर्वत के कुछ हिस्सों पर पड़े बर्फ को भी पिघला दिया। इसके कारण आई भारी बाढ़ ने कई सडक़ों, पुलों और पानी की आपूर्ति व्यवस्था को बर्बाद कर दिया।
एक साल पहले ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी ही बारिश हुई जिसे वहाँ के राजनेताओं ने ‘रेन बॉम्ब’ यानी बारिश बम का नाम दिया था। इसमें 20 लोगों की जान गई थी और हजारों को बचाना पड़ा था।
वैज्ञानिकों ने इन सारी घटनाओं को वायुमंडलीय नदियों का ही परिणाम बताया जो अधिक तीव्र, लंबी, चौड़ी और अक्सर विनाशकारी होती जा रही हैं।
नासा का भी कहना है कि वायुमंडलीय नदियां दुनिया भर में लाखों लोगों को बाढ़ के खतरे में डाल रही हैं।
जर्मनी में पॉट्सडैम विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान संस्थान के अभी हाल के अध्ययन में पता चला है कि वायुमंडलीय नदियों जैसी स्थिति उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में लंबे समय तक चल रही है।
इसका मतलब है कि इससे होने वाली बारिश जमीन पर विनाशकारी हो सकती है।
संयुक्त अरब अमीरात में ख़लीफ़ा विश्वविद्यालय के एक अन्य अध्ययन के मुताबिक़, 2023 के अप्रैल में मध्य पूर्व में भी ठीक ऐसा ही हुआ था।
अध्ययन में निकले निष्कर्ष के मुताबिक़, प्रयोग में लाए गए हाई रेसोल्यूशन सिमुलेशन ने वायुमंडलीय नदियों की उपस्थिति की पुष्टि की जो जो उत्तर-पूर्वी अफ्रीका से पश्चिमी ईरान में तेज गति से आगे बढऩे के कारण भारी बारिश करती थीं।
इनसे होने वाले विनाशकारी बाढ़ों और भूस्खलन के खतरों को देखते हुए, एटमॉस्फेरिक रीवर्स को समुद्री तूफानों की तरह ही उनकी विशालता और तीव्रता के आधार पर पांच प्रकार में श्रेणीबद्ध किया गया है।
हालांकि ये सभी विनाशकारी नहीं होती हैं, खासकर वे, जिनकी तीव्रता कम होती है।
कुछ तो उन इलाकों के लिए बहुत लाभकारी होती हैं जहां लंबे समय तक सूखा रहा हो।
लेकिन यह फ़ेनामिना तेजी से गर्म होते वायुमंडल के लिए चेतावनी है, जो अतीत के मुकाबले अधिक भाप को अपने अंदर समाहित कर रहा है।
वायुमंडलीय नदियों से संबंधित डेटा की कमी बड़ी चुनौती
इस समय दक्षिण एशिया में इस तूफ़ान को लेकर, मौसम की अन्य घटनाओं, जैसे पश्चिमी विक्षोभ या भारतीय चक्रवात की तुलना में अध्ययन हो रहे हैं जो बाढ़ और भूस्खनल की बड़ी घटनाओं का कारण बनते हैं।
आईआईटी इंदौर से जुड़ी एक रीसर्च स्कॉलर रोज़ा वी लिंग्वा के अनुसार, ‘मौसम वैज्ञानिकों, जल वैज्ञानिकों और जलवायु वैज्ञानिकों के बीच प्रभावी सहयोग की कोशिशें मौजूदा समय में चुनौतीपूर्ण हैं क्योंकि इस क्षेत्र में अवधारणा नई है और इसे लागू करना मुश्किल है।’
वो जोड़ती हैं, ‘लेकिन भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है, ऐसे में इस तूफ़ान और इसके विनाशकारी प्रभावों का अध्ययन करना और अहम हो गया है।
वायुमंडलीय नदियों की पहुँच भी नए स्थानों तक हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार, इसका एक कारण बदलते जलवायु में हवा का बदलता बहाव और जेट धाराएँ हैं।
चिली के वालपराइसो विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डेनिज बोजकर्ट के मुताबिक़, ‘हवाओं और जेट धाराओं में बढ़ी हुई लहरों का मतलब साफ़ होता है उनके अपने बहाव के विशिष्ट रास्तों से मोड़ और विचलन। इससे वायुमंडलीय नदियों को अधिक कठिन मार्गों का पालन करने के कारण संभावित रूप से विभिन्न क्षेत्रों पर उनकी अवधि और प्रभाव बढ़ सकता है।
वालपराइसो विश्वविद्यालय के बोजक़र्ट का आगे और कहना है ‘क्षेत्रीय मौसम संबंधी पूर्वानुमानों में वायुमंडलीय नदियों की अवधारणाओं के बारे में जागरूकता सीमित है।
इसका मुख्य कारण और चुनौती विशेष रूप से जटिल इलाकों में वायुमंडलीय नदियों से संबंधित डेटा की कमी है।(bbc.com/hindi)