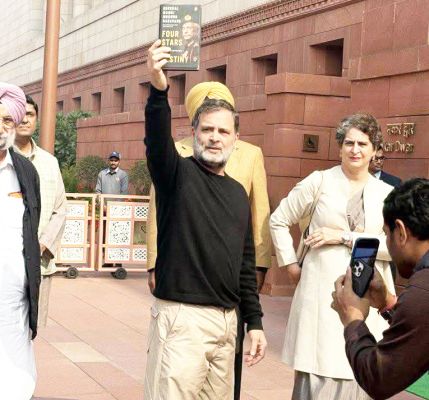विचार / लेख

-द्वारिका प्रसाद अग्रवाल
कैंसर की जड़ें मेरे शरीर में पनप चुकी थी. अन्तत: 2002 में मैं उसकी गिरफ्त में आ गया। कैंसर का नाम सुनते ही इन्सान घबरा जाता है। घबराने की असल वजह होती है- डर। यह बीमारी जरा नखरीली है, मानी तो मानी और न मानी तो सता-सता कर मारती है। लोग इस बीमारी का नाम सुनकर ही सदमा खा जाते हैं, ‘साइलेन्ट हार्ट अटैक’ तो हो ही जाता है. सुनते साथ ही आँखों के सामने मृत्यु का तांडव नृत्य आरम्भ हो जाता है। जैसे ही इस बीमारी के समाचार का आगमन होता है, अनेक विद्वान सलाहकारों का अपने-आप अभ्युदय हो जाता है. सब के सब कैन्सर ठीक होने का मुफ़ीद इलाज बताते हैं- एकदम ‘गेरेन्टीड’, न ठीक होने पर सलाह वापस ! जैसे, गौ-मूत्र, स्वमूत्र का सेवन; गेहूँ के ज्वारे का रस, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक उपचार आदि लेकिन मैं असमंजस में था कि क्या करूं, किसकी शरण में जाऊं ? सबसे अधिक डर इस सूचना का था - ‘किसी हालत में ‘सर्जरी’ मत करवाना क्योंकि चाकू के लगते ही कैन्सर शरीर में बुरी तरह फैलता है।’
मेरा जी घबरायमान हो रहा था. हमारी बिटिया संगीता और भावी दामाद डॉ. केदारनाथ मेरी सर्जरी के पक्ष में थे और वह भी तुरन्त क्योंकि देर करने से कैन्सर के शरीर के अन्य अंगों में फैलने का डर था लेकिन मैं तो त्रिकोणीय समस्या से जूझ रहा था। पहला कोण था- 15 फरवरी को संगीता का विवाह, दूसरा कोण- विवाह के एक माह पूर्व कैन्सर की सर्जरी और तीसरा कोण- देर हो जाने पर कैन्सर के फैलने का डर। अब, आपको तो मालूम है ही कि इस संसार में बिना पैसे कुछ होता नहीं है और मेरी माली हालत इतनी खराब थी कि ‘क्या नहाएं, क्या निचोएं !’
सर्जरी की तारीख नज़दीक आते जा रही थी और अपनी जेब खाली थी, मैं निरुपाय था, चुपचाप अपनी बीमारी के डर को सीने में छुपाए सहज बने रहने की कोशिश करता। मेरा दिमाग दिनोंदिन सुन्न पड़ते जा रहा था, हर दिन मेरे लिए कठिन होता जा रहा था। उसी दौरान एक दिन जब मैं अपनी लॉज में बैठा था, मेरे अभिन्न मित्र रमाकान्त मिश्रा (राजा) जो भारतीय स्टेट बैंक से स्वैच्छिक अवकाश ले चुके थे, आए. हम दोनों ने साथ-साथ चाय पी। उन्होंने पूछा- ‘कब निकल रहे हो, इन्दौर के लिए ?’
‘अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं बना।’ मैंने कहा.
‘अरे, तुझे सर्जरी के लिए निकलना था न ?’
‘सर्जरी मुफ्त में होती है क्या ?’
‘कितना लगेगा?’
‘क्या पता, लेकिन एक लाख से कम क्या लगेगा?’
‘फिर?’
‘फिर क्या...चुपचाप बैठा हूँ.’ मैंने बताया. बैठक समाप्त हो गई।
रमाकान्त चले गए। लगभग दो घंटे बाद आए और मुझे एक बंडल दिया और कहा- ‘ये बहत्तर हजार हैं, इसे लेकर कल सुबह इंदौर के लिए निकल जा, एक दिन की भी देर नहीं करना। मेरे खाते में अभी इतना ही था। और पैसे की ज़रूरत होगी तो मुझे वहां से फोन करना, मैं खुद लेकर आऊंगा।’ उन्होंने मुझे आदेश जैसा दिया और चले गए।
उन रुपयों को देखकर मेरी आंखे डबडबा गई, मैं सोच रहा था- मौत की ओर तेजी से कदम बढ़ाते इन्सान की भला कौन ऐसी मदद करता है !
(रमाकांत मिश्र अब न रहे लेकिन उनकी और उनके दोस्ताना जज्बे की बहुत याद आती है)
(आत्मकथा : ‘दुनिया रंग बिरंगी’ का एक अंश)