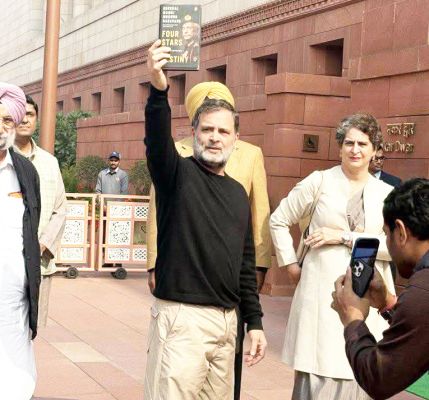विचार / लेख

-डॉ. संजय शुक्ला
हिंदी में एक प्रसिद्ध मुहावरा है ‘पानी -पानी होना’ अर्थात शर्मसार होना यह उक्ति हमारे शहरों के हालात पर सटीक बैठती है। राजधानी दिल्ली से एक बेहद दुखद खबर आई कि वहां के राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भरने के कारण एक छात्र एवं दो छात्राओं सहित तीन युवाओं की मौत हो गई। इस खबर ने एक बार फिर से भारतीय शहरों के सीवरेज व्यवस्था और आपदा प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी। आपदा में भी सियासत का अवसर ढूंढने की प्रवृत्ति वाले इस देश में इस हादसे के बाद एक बार फिर से राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। शर्मसार करने वाली इस सियासत के बीच अहम सवाल यह कि इस हादसे में जिन तीन घरों का चिराग बुझा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिरकार ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे? शायद! इसका जवाब हमारे तथाकथित भाग्य विधाताओं के पास फिलहाल नहीं है। अलबत्ता यह पहला मौका नहीं है जब बारिश के दौरान देश के महानगर और बड़े शहर व्यवस्था और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हों।अमूमन हर मानसून में महज कुछ घंटों की बारिश में हमारे शहरों में ट्रैफिक जाम,जलभराव, जमीन धसकने और बिजली करंट फैलने जैसी घटनाएं अब आम हो चुकी है। बड़े से लेकर छोटे शहरों में बारिश के दौरान बदहाल व्यवस्था का खामियाजा आम नागरिकों को ही भुगतना पड़ता है। देश में एक तरफ ‘स्मार्ट सिटी’ का ढिंढोरा पीटा जा रहा है लेकिन दूसरी ओर मानसून दर मानसून शहरों की हालत बद से बदतर होते जा रही है।गौरतलब है कि साल 2017 में मुंबई में भारी बारिश के दौरान खुले मेन होल में गिरने और डूबने से सुप्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. दीपक अमरापुरकर की मौत ने एक बार लोगों को झंझोड़ कर रख दिया था लेकिन इसके बाद फिर से वही ढाक के तीन पात वाली कहावत चरितार्थ हो रही है।
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) के एक शोध में बताया गया है कि देश के 66 फीसदी शहरों में शहरी विकास के लचर योजनाओं के चलते बारिश के दौरान बाढ़ और जलभराव का खतरा बना रहता है फलस्वरूप इन शहरों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते दस सालों के दौरान जलभराव तथा क्षतिग्रस्त सडक़ों के मरम्मत व निर्माण के चलते देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को लगभग 14 हजार करोड़ रुपए तथा चेन्नई को 25 हजार करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को बीते साल 2023 के मानसून में बाढ़ और जलभराव की वजह से 10 हजार करोड़ तथा बेंगलुरु को 225 करोड़ का नुकसान हुआ है। बहरहाल शहरों में बाढ़ और जलभराव का असर केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं पड़ रहा है बल्कि इस दौरान आम नागरिकों की भी दिक्कतें काफी बढ़ जाती है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक जहां 68 फीसदी नागरिकों ने बताया कि जलभराव के चलते सडक़ हादसों का जोखिम बढ़ जाता है वहीं 64 फीसदी लोगों की नौकरी और काम के घंटों में असर पड़ता है। शहरों में जल निकासी और साफ-सफाई की माकूल व्यवस्था नहीं होने का असर जनस्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। आम तौर पर नाले-नालियों में बरसाती पानी के जमाव, सीवरेज व साफ सफाई व्यवस्था की नाकामी की वजह से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे मच्छर जनित रोगों के साथ ही पीलिया,आंत्रशोथ, टायफाइड सहित आंख और त्वचा से संबंधित रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बहरहाल शहरों में बारिश के दौरान जलभराव समस्या का प्रमुख वजह शहरों के वाटर बॉडी यानि तालाबों का खत्म होना, बढ़ता कांक्रीटीकरण और सीवेज लाइनों में तकनीकी खामियां हैं। शहरीकरण, व्यवसायीकरण और अव्यवस्थित बसाहट के चलते शहरों से तालाब लगातार खत्म हो रहे हैं अथवा इनका क्षेत्रफल घट रहा है जबकि इन तालाबों में ही बारिश का पानी इक_ा होता था। शहरों में कांक्रीट के सडक़ों, फूटपाथ और रिहायशी तथा व्यवसायिक इमारतों के चलते जमीन द्वारा बरसात की पानी सोखने की क्षमता कम होते जा रही है। पुराने शहरों में सीवेज सिस्टम आज भी दशकों पुराने हैं जो गाद और अतिक्रमण के चलते तेज बारिश के समय पानी को ड्रेन करने में नाकाम हैं फलस्वरूप जलभराव की स्थितियां निर्मित हो रही है। इसके अलावा शहरों में जलभराव के लिए आम नागरिक भी जवाबदेह हैं जो पॉलिथीन बैग, प्लास्टिक सामाग्रियों और कचरों को नालियों में डालते हैं फलस्वरूप नालियां जाम हो जाती है। बहरहाल भारत के शहर सिर्फ मानसून में ही बदहाल नहीं हैं बल्कि बाकी महिनों में भी अमूमन हालात एक जैसे हैं। यह हालात तब है जब इन शहरों को विश्व स्तरीय बनाने के नाम पर सरकार और शहरी प्रशासन के जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों का भारी भरकम दल अध्ययन यात्रा के लिए दुनिया के चकाचौंध भरे शहरों का भ्रमण करते हैं। यह स्मरण में नहीं है कि किसी भी सरकार या नगरीय निकाय ने अपने विदेश यात्रा के बाद वहां के योजनाओं को देश और शहर में लागू करने के लिए कोई योजना बनाई हो यानि कुल मिलाकर यह तथाकथित अध्ययन यात्रा जनता के पैसों से सैर-सपाटे का जरिया भर बन रहा है।
गौरतलब है कि किसी भी देश के मजबूत अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब उसका चमचमाता शहर ही होता है, शहर जहां तरक्की, रचनात्मकता और नवीनता का केंद्र होता है वहीं यह अर्थव्यवस्था में प्रगति और रोजगार का जनक भी होता है।? भारत के कुल जीडीपी में शहरों का योगदान 63 फीसदी है। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही लोगों के लिए महानगरीय और शहरी जीवनशैली हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है लेकिन हाल के वर्षों में हमारे शहर तमाम विसंगतियों से जूझ रहे हैं। देश के ज्यादातर शहरों में अवैध कॉलोनियों और स्लम बस्तियों की बाढ़ आ गई है। बिलाशक इसके लिए भ्रष्टाचार और वोट बैंक की सियासत ही प्रमुख वजह है। आलम यह है कि अनियोजित विकास और जनसंख्या के बढ़ते दबाव के चलते हमारे शहर हांफने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने शहरों की शक्ल- सूरत और सीरत संवारने के लिए साल 2015 में देश में ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ का आगाज किया था। योजना के तहत पांच चरणों के बाद चुने गए 100 शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ इन शहरों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहरी जनजीवन के गुणवत्ता में सुधार,सुरक्षा और संचार प्रौद्योगिकी का विकास, गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य और पेयजल व्यवस्था की सुनिश्चितता और जनभागीदारी से सरकारी कामकाज में सुधार जैसे उद्देश्य भी निर्धारित किए गए थे। अलबत्ता अब इस योजना की अवधि पूरा होने की है लेकिन इस योजना में शामिल अधिकांश शहर अभी भी स्मार्ट सिटी के लक्ष्य और मानकों से कोसों दूर है। योजना में शामिल शहरों की पहचान अब भी गढ्ढे और धूल की बनी हुई है जिसका खामियाजा शहरवासियों को चुकाना पड़ रहा है।
देश के चुनिंदा शहरों को छोड़ दें तो अधिकांश शहर साफ पेयजल, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। अलबत्ता मोदी सरकार की शहरों को स्मार्ट बनाने की महत्वाकांक्षी योजना कछुआ चाल से चल रही है। दूसरी ओर इस योजना में भ्रष्टाचार, फिजूलखर्ची और गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों की खबरें जनता के अरमानों पर लगातार पानी फेर रही है। शहरों की स्थिति देखने के बाद रहवासी यही उलाहना दे रहे हैं कि गोया स्मार्ट सिटी की बात छोडि़ए इन्हें रहने लायक ही बना दीजिए। भारतीय शहरों की प्रमुख समस्या यातायात और पार्किंग, नाकाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाहनों की बढ़ती संख्या, झुग्गी और मलिन बस्तियां, बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण, अतिक्रमण, बिजली आपूर्ति,अवारा मवेशियों का जमावड़ा, लचर सीवरेज सिस्टम और वेस्ट मैनेजमेंट, कचरों का पहाड़,बढ़ती आर्थिक असमानता और अपराध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 14 शहर शामिल हैं। स्विस कंपनी आईक्यू एयर के शोध के मुताबिक विश्व के टॉप 100 प्रदूषित शहरों में से 65 भारतीय शहर हैं।
दरअसल पर्यावरण प्रदूषण ने शहरी नागरिकों का जीना मुहाल कर दिया है जिसके लिए शासन, नगरीय प्रशासन और नागरिक भी जवाबदेह हैं। आम भारतीय शहर वायु,जल और ध्वनि प्रदूषण के गिरफ्त में है जिसका असर जनस्वास्थ्य पर पड़ रहा है। शहरों में चूल्हे या सिगडिय़ों, वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले धुंआ और अधोभूत संरचना विकास तथा निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल पर्यावरण कानूनों को धता बता रही है।कार्बनयुक्त धुंआ और धूल से एक बड़ी आबादी श्वसन तंत्र से लेकर एलर्जी, चर्मरोग और कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों का सामना कर रही है। शहरों में कल-कारखानों और व्यक्तिगत वाहनों की संख्या में इजाफा होने के कारण ध्वनि प्रदूषण जनस्वास्थ्य के लिए खतरा बने हुए हैं। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, दफ्तरों और घरों में एयरकंडीशनर के बढ़ते उपयोग तथा पेड़ों के अंधाधुंध कटाई के कारण शहरों के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यह अतिश्योक्ति नहीं होगी कि देश के शहर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से जवाबदेह हैं।
गौरतलब है कि आर्थिक उदारीकरण और ग्रामीण विकास की अनदेखी के कारण भारत में शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की रफ्तार काफी तेज हुई है।
रोजगार की तलाश में लोगों का गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ा है। भारत शहरीकरण के मामले में विश्व का दूसरा बड़ा देश है जहां 5000 से ज्यादा बड़े और छोटे शहर हैं। इनमें 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 53 शहर हैं जिसके साल 2030 तक 70 तक पहुंचने की संभावना है।शहरों के ज़द में आने वाले गांव भी अब शहरों का हिस्सा बन रहे हैं लेकिन इस अनुपात में सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध नहीं है। भारत जैसे विकासशील और कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश में शहरों का सुनियोजित विकास सरकार के लिए बड़ी चुनौती है इस चुनौती से निबटने के लिए जनभागीदारी आवश्यक है। शहरी समस्याओं के निर्मूलन के लिए जहां सरकारी तंत्र और स्थानीय प्रशासन को दृढ़ इच्छाशक्ति प्रदर्शित करनी होगी वहीं नागरिकों को भी अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति सजग होते हुए स्व अनुशासन पर जोर देना होगा। सरकारी तंत्र को अपने कार्यों में पारदर्शिता और प्रतिबद्धता बरतनी होगी ताकि जनसामान्य को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं सुलभ हो सके आखिरकार जनता इसके लिए अपने जेब से टैक्स अदा करती है।
बिलाशक शहरों की दुर्दशा के लिए जितना जिम्मेदार सरकारी तंत्र है उतना ही जवाबदेह आम नागरिक भी हैं। शहरों को स्मार्ट बनाने की होड़ में जिम्मेदार लोग अनेक अव्यवहारिक और अदूरदर्शिता पूर्ण फैसला ले रहे हैं। ऐसे फैसलों में नदियों और तालाबों के सौंदर्यीकरण के नाम पर वाटर बॉडी को पाटकर चौपाटी लगाने और बोटिंग जैसी योजनाएं हैं जो इन जलस्रोतों के रिचार्ज क्षमता को घटा रही हैं वहीं फूड स्टालों के सड़े-गले अपशिष्टों की वजह से इनका इकोसिस्टम भी प्रभावित हो रहा है। शहर के नीति निर्धारकों को नदियों, तालाबों,उद्यानों, शिक्षण संस्थानों और खेलकूद मैदानों के व्यवसायिक उपयोग से बचना चाहिए। शहरों के प्रति नागरिकों में भी स्वानुशासन की काफी न्यूनता दृष्टिगोचर हो रही है। इसका अदद उदाहरण सिंगल यूज़ प्लास्टिक का नागरिकों द्वारा किए जा रहे धड़ल्ले से इस्तेमाल का है जबकि सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इसे पर्यावरण के लिहाज से प्रतिबंधित किया है। बहरहाल शहरवासियों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर पाबंदी, कचरा प्रबंधन,जल और वृक्ष संरक्षण, अधिकाधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के उपयोग तथा निजी वाहनों के फिटनेस जैसे सामुदायिक जवाबदेही के प्रति अनुशासित होना होगा तभी हमारे शहर रहने लायक बन सकेंगे।