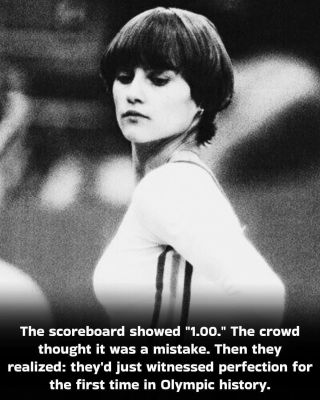विचार / लेख

-कनक तिवारी
1. प्रशांत भूषण के अवमानना प्रकरण के कारण जिरह में संविधान के इतिहास और उसकी भविष्यमूलकता को लेकर कई तरह के पेंच और द्वैध पैदा हो गए हैं। उनकी भू्रणहत्या नहीं की जानी चाहिए। ये सवाल फिलहाल तो जस्टिसगण अरुण मिश्रा,बी आर गवई और कृष्ण मुरारी की बेंच में आश्वस्ति मांग रहे हैं कि उन पर ‘पब्लिक डोमेन’ में बहस सुनी जाए। संविधान न्यायालय भी दरबार-ए-खास नहीं दरबार-ए-आम होते हैं। सभी संस्थाओं की लोकतांत्रिक बादशाहत में संवैधानिक तेवर होना भी ज़रूरी है। प्रशांत भूषण पर चल रहे अवमानना मामले ने देश क्या दुनिया के समझदार नागरिक वर्ग में चिंताजनक और चिन्तनीय बौद्धिक खलबली मचा रखी है। लोग सीधे संविधान से ही सवाल पूछ रहे हैं कि तुम्हारी उद्देशिका में ही लिखा है न कि ‘हम भारत के लोग’ ही संविधान निर्माता हैं। ‘हम भारत के लोग’ ही सार्वभौम हैं। न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न संसद और न खुद संविधान ही सार्वभौम है। इसलिए संविधान के रचयिता खुद अपने लिखे के पाठ संविधान, अर्थात अपने खुद के विवेक से ‘पब्लिक डोमेन’ में खुली जिरह करने के लिए सक्रिय होकर आश्वस्त हैं।
2. तथ्यात्मक मुद्दा इतना ही है कि प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के बहुत सक्रिय वकील हैं। अपनी अलग पहचान बनाते जनहित के मामले उठाते वकीलों में लगभग अव्वल हैं। उन्होंने कई बार ऐसा भी कुछ कहा और किया भी है जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत उन पर अवमानना प्रकरण कायम हुए हैं। मेधा पाटकर, अरुंधति रॉय और प्रशांत भूषण ने ‘नर्मदा बचाओ आंदोलन’ के सिलसिले में विस्थापितों के पक्ष में भाषण और वक्तव्य देते सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना भी दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों की शिकायत पर तीनों के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दर्ज हुआ। प्रशांत भूषण और मेधा पाटकर के खिलाफ कार्यवाही नहीं की लेकिन ख्यातिप्राप्त लेखिका अरुंधति रॉय ने नोटिस के जवाब में सुप्रीम कोर्ट की समझ के अनुसार ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो अवमाननाकारक लगी। जिन भाषणों के आधार पर मुकदमा था वे तो अलग थलग हो गए। नतीजतन अरुंधति को सजा दी गई। केरल के प्रसिद्ध मुख्यमंत्री ई. एम. एस. नम्बूदिरीपाद को न्यायपालिका की अकादेमिक आलोचना करने के कारण में सजा दी गई। अजीबोगरीब कारण बताया गया कि उनकी और उनके विख्यात वकील वी. के. कृष्णमेनन की न्यायपालिका को लेकर माक्र्स और एंजिल्स के विचारों के अनुरूप भाषण देने का दावा सही नहीं है। देश के कानून मंत्री पी. शिवशंकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आलोचना में कह गए कि दहेजलोभी लोग बहुओं को जला रहे हैं, काले बाजारिए, भ्रष्ट लोग और विदेशी विनिमय वगैरह के अभियुक्त भी सुप्रीम कोर्ट में स्वर्ग पा लेते हैं। चीफ जस्टिस सव्यसाची मुखर्जी ने उसे एक विधिशास्त्री का ‘एप्रोच’ और ‘एटिट्यूट कहा, ‘लेकिन सजा नहीं दी। 1919 में अंगरेज जज ने ‘यंग इंडिया’ के सम्पादक गांधीजी को बार बार माफी मांगने का कहने पर भी गांधी के माफी नहीं मांगने पर भी सजा नहीं दी। केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया। गांधी ने साफ कह दिया था वे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई अदालती अंकुश स्वीकार नहीं करते। जज जो चाहे सो सजा दे दे।
एक जज हेवार्ड ने उन्हें और प्रकाशक महादेव देसाई को सत्याग्रही मान लिया था। कई मामलों में निहित न्याय सिद्धांतों को अपने लंबे चैड़े जवाब और सैकड़ों पृष्ठों के दस्तावेजों के साथ प्रशांत भूषण ने विचारण के लिए तीन जजों की बेंच के सामने दाखिल किया। मजा यह कि आठ दस दिनों में ही उन जवाबी बिंदुओं और दस्तावेजों को मुनासिब प्रक्रिया के चलते बहुत कम समय में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समझ में 108 पृष्ठों का आदेश पारित करते प्रशांत भूषण को जिम्मेदार ठहरा दिया। उनको कितनी सजा दी जाए केवल इस पर विचार होना है। प्रशांत भूषण के वकील डॉ. राजीव धवन ने यह भी कह दिया कि उसमें से कई पृष्ठ तो किसी अन्य मामले से शब्दष: उठा लिए गए लगते हैं।
3. संविधान सभा में नागरिकों के मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से हूबहू उधार लिए गए हैं। अभिव्यक्ति के नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते संविधान सभा में कई आधारों सहित मानहानि और अदालत की अवमानना के संबंध में संसद को अधिनियम बनाने के अधिकार दिए गए। हालांकि दमदार सदस्य आर. के. सिधवा और विश्वनाथ दास ने ऐसी कड़ी बातें कही थीं कि आज कोई कह नहीं सकता। वरना सीधा सीधा अवमानना का मामला बन जाएगा। प्रशांत भूषण ने तो वैसा कुछ नहीं कहा। उन सदस्यों ने तो यहां तक कह दिया था कि जज भी आखिर मनुष्य ही होते हैं। उनके सिर पर दो सींग नहीं होते। उनसे भी गलतियां होती हैं। कई कंगाल वकील तक जज बना दिए जाते हैं। आजादी के बाद भी जजों की ब्रिटिश हुकूमतशाही के वक्त की मानसिकता कायम चली आई है।
बहरहाल प्रतिबंध तो अनुच्छेद 19 (2) में लगा ही वह कहता है, ‘‘19. वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण-(2) खण्ड (1) के उपखण्ड (क) की कोई बात उक्त उपखण्ड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय-अपमान, मानहानि या अपराध-उद्दीपन के सम्बन्ध में युक्तियुक्त निर्बंन्धन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नही करेगी।’’
21 साल की उम्र में ही प्रशांत भूषण ने आपातकाल के वक्त ‘दी केस दैट शूक इंडिया’ नामक किताब लिख दी थी।
4. प्रशांत भूषण में युवकोचित बौद्धिक गुस्सा भी रहता है। मनुष्य में विचार उसके संस्कार, पैतृक गुण, सामाजिक हैसियत आदि के कारण सार्वजनिक अभिव्यक्तियों में वाचाल रहते है। मानो अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि पी. शिवशंकर ने कहा था कि न्यायपालिका में उच्च वर्णों और वर्गों की दबंगई होने से वहां वंचितों की वेदना का फलसफा सूखा सूखा सा है। यही तो जस्टिस कर्णन को अदालत की अवमानना पर सजा होने से कई बुद्धिजीवी कह रहे हैं। न्यायिक इतिहास के भीष्म पितामह शताब्दी पुरुष जज वी. आर. कृष्ण अय्यर ने रिटायरमेंट के बाद कह दिया था कि न्यायपालिका तो अस्तित्वहीन संस्था हो गई है। वहां ईसा मसीह को तो सूली पर चढ़ाया जाता है लेकिन खलनायकों को नहीं। कई बार उसका सभ्यता से भी संस्पर्ष बिछुड़ जाता है। उन पर भी मुकदमा दायर किया गया लेकिन केरल के चीफ जस्टिस रहे सुब्रमणियम पोट्टी की बेंच ने नोटिस तक देने की जरूरत नहीं समझी। कहा कि न्यायपालिका की छाती इतनी चैड़ी होनी चाहिए कि वह सवालों को अपने विवेक से सुलझाती रहे। अमेरिका और इंग्लैंड में भी जजों को मीडिया में मूर्ख और बूढ़ा तक कहकर उनका सिर नीचे और पैर ऊपर दिखाते तस्वीरें छाप दी गई हैं। वहां भी शिकायतकुनिंदा पहुंचे लेकिन उन्हीं जजों ने साफ किया कि यह तो सच है कि हम बूढ़े हैं। कोई हमें बेवकूफ समझ रहा है। तो यह तो उसकी निजी राय है, हमारी अपने बारे में ऐसी राय नहीं है।
5. 2009 में प्रशांत भूषण के कहने के वक्त कि पिछले छ: वर्ष के दौर में न्यायपालिका में लोकतंत्र का क्षरण हुआ या पिछले चार मुख्य न्यायाधीषों के वक्त भ्रष्टाचार रहा है, सोषल मीडिया सक्रिय होकर आया नहीं था। अरुंधति के पक्ष में भी देश के सैकड़ों बुद्धिजीवी और विदेशों के प्रख्यात विद्वान और सांसद वगैरह सुप्रीम कोर्ट को लिख चुके थे कि अदालती अवमानना को लेकर संवैधानिक अधिकारों की समझ को ही तो अरुंधति ने अपने जवाब में विन्यस्त किया है। वह अवमानना का नहीं बौद्धिक वादविवाद का मामला है और पूरी तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी के तहत है। नॉम चॉम्की जैसे विख्यात बुद्धिजीवी, पत्रकार, राजनेता, प्राध्यापक जिनमें ‘हिन्दू’ के संपादक एन. राम, ‘जनसत्ता‘ के संपादक प्रभाष जोशी और न जाने कितने लोग शामिल थे सामने आए। जिस जज ने मामला पंजीबद्ध कर नोटिस जारी की थी, अरुंधति ने सवाल उठाया था कि उन्हें नोटिस के जवाब की सुनवाई अन्य जज से करानी चाहिए, तभी वस्तुपरक आकलन होगा। लेकिन जस्टिस जी. बी. पटनायक ने दलील नहीं मानी।
6. हालिया कोविड-19 के भयानक प्रकोप के दौर में चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की अपने गृहनगर नागपुर पहुंचकर पचास लाख रुपये की भाजपा कार्यकर्ता की विदेशी हारले डेविडसन की मोटरसायकल पर बैठकर तस्वीर खींची गई। वह सोशल मीडिया में वायरल हो गई। हजारों नागरिकों ने तरह तरह की असहज क्या भद्दी और अपमानजनक टिप्पणियां कर दीं। प्रशांत भूषण ने भी शायद इस आशय का ट्वीट कर दिया होगा कि न्याय मिलने की मुश्किलों के इस महामारी के दौर में सुप्रीम कोर्ट में त्वरित और जरूरी सुनवाई के वक्त ऐसी फोटो खिंचाने और संपूर्ण व्यापक न्यायिक व्यवस्था के आचरण का आकलन करने से आने वाली पीढिय़ां भारतीय न्यायपालिका के बारे में क्या धारणाएं कायम करेंगी। कुछ शिकायतखोर नस्ल के वकीलों का कानूनी ज्ञानशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रेखांकित होता रहता है। एक शिकायत के आधार पर प्रशांत भूषण को अवमानना का नोटिस आननफानन में मिला। तुर्रा यह कि 2009 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों के खिलाफ जो कथित कटाक्ष किया था, उसे भी सुनवाई के लिए साथ साथ सूचीबद्ध कर दिया गया। बहुत कम दिनों में फैसला देने का इरादा तेज प्रक्रिया के चलते इशारों इशारों में ‘कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है‘ की तर्ज पर जाहिर कर दिया गया। अपनी रीढ़ की हड्डी पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ तेजतर्रार वकील संविधान के ज्ञान, फलक और जन-अभिमुखता के विकास के लिए लगातार जजों के कई क्रोधी तेवर झेलते जद्दोजहद कर रहे हैं। अभी भी सब कुछ बरबाद नहीं हुआ है। डॉ. राजीव धवन, दुष्यंत दवे, कोलिन गोन्जाल्वीस, इंदिरा जयसिंह, कामिनी जायसवाल, वृंदा ग्रोवर जैसे प्रसिद्ध वकीलों ने कई सवाल उठाए हैं। न्यायिक प्रक्रिया की हड़बड़ी में उनका व्यापक विचारण कई बार नहीं हो पाता। यह पहला वक्त है जब एक नागरिक/वकील पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का मामला चलाने का खुद संज्ञान इस तेज गति और मति से लिया है लेकिन नेपथ्य से प्रॉम्पिटंग की कई आवाजें फुसफुसाती हुई लग रही हैं। संविधान के अंतरिक्ष में अब अनसुनी कैसे हो सकती है? प्रशांत भूषण द्वारा दिए गए जवाब पर कोई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के चलते नहीं की जानी चाहिए। वह तो तीन सदस्यीय पीठ के जेहन में है ही।
7. पहली बार लेकिन कुछ नए सवाल पैदा हुए हैं। सोशल मीडिया की वजह से जन-इजलास में इन मुद्दों पर बातचीत करना संभव और जरूरी है। वह बातचीत संविधान के निर्माता ‘हम भारत के लोग’ कर सकते हैं। इन्हें सारसंक्षेप में समेटा जा सकता है:
(1) अरुंधति के समर्थन में सैकड़ों बुद्धिजीवियों की राय को इसलिए दरकिनार किया गया होगा क्योंकि वे ‘बाहरी व्यक्ति’ थे। उनकी राय अकादेमिक लगने से संविधान के इस्तेमाल के अनुभवों की विशेषज्ञता की नहीं रही होगी। प्रशांत भूषण के मामले में जस्टिस चीफ जस्टिस रहे राजेन्द्रमल लोढ़ा ने (जिनकी अध्यक्षता के कॉलेजियम में मौजूदा तीन सदस्यीय पीठ के मुखिया जज की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी) तो कह दिया है कि कोविड-19 की महामारी के चलते यह महत्वपूर्ण मामला ‘वर्चुअल कोर्ट’ के जरिए निपटाने की क्या ज़रूरत थी? उसे महामारी के बाद औपचारिक भौतिक अदालती प्रक्रिया के तहत निपटाने से बहुत कुछ कहने सुनने की स्थिति बनती। इंग्लैंड से भारत ने संवैधानिक ज्ञान उधार लिया है। वहां की पुष्ट परंपराएं कहती हैं ‘न्याय केवल होना नहीं चाहिए। वह होता हुआ दिखना भी चाहिए।’ बिना आपातकाल लगाए और अब तो मैदान में लाए गए (गोदी?) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ गलबहियां करते प्रिंट मीडिया बेतरह, बेवजह चुप है। प्रशांत भूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की चिंतातुर व्याकुलता पर साजिशी चुप्पी साधकर जैसे सेंसर लगा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का मामला मीडिया के अंतरिक्ष में नया उपग्रह बनाकर उछाला गया है। उस घटना का इतना प्रचार है कि भारत में चीन की घुसपैठ, लाखों लोगों का कोरोना में मरना खपना और सदा मीडिया के फोकस में रहने वाले बेचैन प्रधानमंत्री तक के लिए जगह और समय की कमी हो रही है। संविधान सभा ने कभी नहीं सोचा होगा कि मीडिया (तब प्रेस कहा था) जनता के मुद्दों तो क्या मुंह पर सेंसर लगा देगा। जनअभिव्यक्तियों के खिलाफ लिख और कुचलकर सत्ता प्रतिष्ठान का बगलगीर बनेगा। फिर भी नागरिकों के बराबर आजादी पा लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारों के तहत जनता और न्याय हित में कई अदालती प्रक्रियाओं की खबरों को मीडिया में प्रकाशित होने से रोका है। सुप्रीम कोर्ट को यह अजूबा भी तो देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट खुद नागरिक आज़ादी के अहम सवाल से जूझते अपने ही वरिष्ठ रहे पूर्व जजों की राय तक को मीडिया में नहीं पढ़ या सुन पा रहा हो। तब क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया नहीं होता तो इस मामले की जनसरोकारिता की ही मौत हो जाती!
(2) चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के वक्त जनवरी 2018 में वरिष्ठ जजों रंजन गोगोई,जे. चेलमेश्वर, मदन बी. लोकुर और कुरियन जोसेफ ने सीधे मीडिया से बात की थी। वह सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का अकेला अपवाद है। उन्होंने खुलकर चीफ जस्टिस पर कई आरोप लगाए। उनमें यह भी था कि चीफ जस्टिस बहुत संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों को भी उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के 24 जजों में से अपेक्षाकृत कनिष्ठ जज की अध्यक्षता की पीठ को दे देते हैं। प्रशांत भूषण के मामले में भी वरिष्ठता का सिद्धांत नहीं, चीफ जस्टिस के अधिकार से वरिष्ठता क्रम के जजों को सौंपा नहीं गया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था मामला देने का चीफ जस्टिस का अधिकार है क्योंकि अंगरेजी परम्परा में वही ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ होता है। अंगरेजी परंपरा में तो वरिष्ठता का भी सिद्धांत रहा है-यह नहीं कहा था। परम्परा में तो यह भी है जिस जज साहब पर भरोसा नहीं हो, तो उन्हें मामले से हट जाना चाहिए। प्रशांत भूषण ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज एच. एस. कपाडिय़ा के कई शेयर एक प्राइवेट कम्पनी स्टरलाइट में रहे हैं। फिर भी वकीलों से उन्होंने स्टरलाइट कम्पनी के मामले में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) थे। इसकी आलोचना प्रशांत भूषण ने खुलकर की। उन्होंने ही प्रशांत भूषण के खिलाफ जजों के भ्रष्टाचार वाले कथन के खिलाफ अवमानना की शिकायत की थी। उसे अभी सुना जा रहा है। किसी भी आरोपी को पूरी सुनवाई का मौका दिए बिना या उठाए गए मुद्दों पर संवैधानिक तुष्टि हासिल किए बिना फैसला नहीं देना चाहिए जजों के अनुसार पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना चाहिए। शुरुआती 5 जज सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के सदस्य होते हैं। जस्टिस रंजन गोगोई के विवादास्पद अपवाद को छोडक़र (जो राम मंदिर के फैसले के बाद राज्यसभा में मनोनीत हुए) तीन वरिष्ठ जजों जस्टिस चेलमेश्वर, मदन बी. लोकुर और कुरियन जोसेफ ने प्रशांत भूषण के पक्ष में खुलकर बयान दिए हैं कि कोई मामला ही नहीं बनता।
(3) जस्टिस कुरियन जोसेफ के तर्क में बहुत दम है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अवमानना करार देकर मामला चलाना चाहे तब भी जब आरोपी कहे मुझे अभिव्यक्ति की अबाधित आजादी है। सच तो यह है यह मामला भारत-चीन की सरहदों की तरह नहीं, माता पिता के प्रेम के बटवारे की सरहद का किसी तरह निर्धारण करे) यही संविधान का बेहद नाजुक बिन्दु है। संविधान निर्माता जनता के भी खिलाफ सुप्रीम कोर्ट न्यायिक व्याख्या का संवैधानिक अधिकारी होने से कोई विपरीत अमलकारी फैसला दे, तो भाष्यकार जनता का क्या होगा? ऐसे (संभावित) विवाद की कल्पना संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, डॉ. भीमराव अंबेडकर और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अगुवाई के करीब 300 सदस्यों को नहीं रही है। इसलिए कुरियन जोसेफ ठीक कहते हैं कि प्रशांत भूषण का मामला कम से कम 5 या अधिक जजों की संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए। उनके अनुसार प्रकरण में कई सैद्धांतिक सवाल निहित हैं। जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। जस्टिस कर्णन के अवमानना मामले में पूरी सुप्रीम की राय के अनुपालन में सात वरिष्ठ जजों की पीठ में सुनवाई होकर फैसला हुआ था। अभी तो उन्हीं में से कुछ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने संयुक्त पत्र प्रशांत भूषण के तर्कों के पक्ष में लिखा है।
(4) कानून यह है कि फौजदारी नस्ल का अवमानना मामला आवश्यकतानुसार अटॉर्नी जनरल की अनुमति के बाद अदालत के सामने रखा जाए। अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15 के अनुसार ‘‘आपराधिक अवमानना की दशा में, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या तो स्वप्ररेणा से या (क) महाधिवक्ता के, अथवा (ख) महाधिवक्ता की लिखित सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति के समावेदन पर कार्रवाई कर सकेगा। स्पष्टीकरण-इस धारा में ‘‘महाधिवक्ता’’ पद से अभिप्रेत है-(क) उच्चतम न्यायालय के सम्बन्ध में, महान्यायवादी या महासालिसिटर।
प्रशांत भूषण के मामले में रजिस्ट्री को या तो संकोच रहा या उसने इस नियम के अनुसार एटार्नी जनरल की राय लेने संबंधी नोट लगाकर जजों के सामने मामला रखा होगा। बेंच ने उसे गैरजरूरी प्रावधान मानते सुनवाई की होगी। अटॉर्नी जनरल से सहमति ले ली जाती तो क्या दिक्कत थी? प्रशांत भूषण ने 2009 में जो कथित अवमाननाकारक बयान दिया, उस मामले में तो अटॉर्नी जनरल की राय ली गई थी। वह मामला 11 साल तक सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में पड़ा रहा। वहां कई मामले अपना अपना दुखड़ा सुनाते, नसीब ढूंढते बिसूरते पड़े रहते हैं। मामला इतना विस्फोटक समझा गया होता तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज और चीफ जस्टिस 2009 से लेकर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के वक्त तक रहे हैं, तब तक सुनवाई क्यों नहीं हुई? मौजूदा चीफ जस्टिस भी 18 नवम्बर 2019 से हैं। तब कोरोना और हारवे मोटर साइकिल वाली दुर्घटना नहीं हुई थी। जो सभी संभावित जज उस मामले को सुन सकते थे। उनमें से ही जज प्रशांत भूषण के पक्ष में खड़े होकर वैधता पर सवाल उठा रहे हैं। इनमें जस्टिस ए. के. गांगुली (2012), चीफ जस्टिस राजेन्द्रमल लोढ़ा (2014), जस्टिस विक्रमजीत सेन (2015), जस्टिस चेलमेश्वर (2018), जस्टिस कुरियन जोसफ (2019), जस्टिस आफताब आलम (), जस्टिस ए. के. गांगुली (2012), जस्टिस मदन बी. लोकुर भी (2018), जस्टिस जी. एस. सिंघवी (2013) कई और जज हैं। सवाल उठ रहे हैं कि हम होते तो क्या फैसला करते? सुदर्षन रेड्डी (2011), जस्टिस गोपाल गौड़ा (2016) रिटायर हो गए हैं। जस्टिस रूमा पॉल भी साथ हैं, जो अलबत्ता 2006 में रिटायर हो गई थीं।
(5) अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल में असाधारण समझ, योग्यता और निष्ठायुक्त आचरण आदर्श है। पहले झिझकते हुए और बाद में साफगोई में उन्होंने बेंच से अनुरोध किया कि प्रशांत भूषण को सजा नहीं दी जाए। अनुरोध भावुक नहीं है। भारत के महान्यायवादी की संवैधानिक समझ का फलसफा है। अटॉर्नी जनरल सरकारी नौकर नहीं होते। असाधारण विद्वता के विधिशास्त्री को संविधान की रक्षा के लिए अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है। वह राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के साथ संविधान में कार्यपालिका का अंग है। ‘‘52. भारत का राष्ट्रपति-भारत का एक राष्ट्रपति होगा।‘‘ ‘‘63. भारत का उपराष्ट्रपति-भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।’’ ‘‘74. राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद्-(1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देनेे लिए एक मंत्रि-परिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।’’ ‘‘76. भारत का महान्यायवादी-(1) राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा। (2) महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय-समय पर निर्देर्षित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। (3) महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्यक्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा।’’
अटॉर्नी जनरल की अनसुनी कर दी गई। इस तरह का सवाल सुप्रीम कोर्ट में पहली बार आया जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते वक्त अटॉर्नी जनरल की राय नहीं ली गई को जरूरी नहीं माना। अटार्नी जनरल से राय नहीं लेने पर भी उनके द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में (?) अनुरोध करने की संवैधानिक स्थिति तय नहीं हुई है। संविधान या अधिनियम खामोश हैं। कहा जा सकता है कि क्या यह भी स्थिति संविधान पीठ के लायक नहीं बनती? फैसला जो हो वह तो संवैधानिक इतिहास का हिस्सा बनेगा।
(6) अवमानना अधिनियम की धारा 19 इस तरह है। 19. अपीलें-(1) अवमान के लिए दण्डित करने की अपने अधिकारिता के प्रयोग में उच्च न्यायालय के किसी आदेश या विनिश्चय की साधिकार अपील-(क) यदि आदेश या विनिश्चय एकल न्यायाधीश का है, तो न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ को होगी। (ख) यदि आदेश या विनिश्चय न्यायपीठ का है, तो उच्चतम न्यायालय को होगी। परन्तु यदि आदेश या विनिश्चय किसी संघ राज्यक्षेत्र के किसी न्यायिक आयुक्त के न्यायालय का है तो ऐसी अपील उच्चतम न्यायालय को होगी। (2) किसी अपील के लम्बित रहने पर, अपील न्यायालय आदेश दे सकेगा कि-(क) उस दण्ड या आदेश का निष्पादन, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, निलम्बित कर दिया जाए। (ख) यदि अपीलार्थी परिरोध में है तो वह जमानत पर छोड़ दिया जाए, और (ग) अपील की सुनवाई इस बात के होते हुए भी की जाए कि अपीलार्थी ने अपने अवमान का मार्जन नहीं किया है। (3) यदि किसी आदेश से, जिसके विरुद्ध अपील फाइल की जा सकती है, व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का समाधान कर देता है कि वह अपील करने का आशय रखता है तो उच्च न्यायालय की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग भी कर सकेगा। (4) उपधारा (1) के अधीन अपील, उस आदेश की तारीख से जिसके विरुद्ध अपील की जाती है। (क) उच्च न्यायालय की किसी न्यायपीठ को अपील की दशा में, तीस दिन के भीतर की जाएगी। (ख) उच्चतम न्यायालय की अपील की दशा में, साठ दिन के भीतर की जाएगी।
कुरियन जोसेफ ने यही बुनियादी सवाल उठाया है। यह न्याय के सिद्धांत और अधिनियम में बड़ी चूक है। अकबर इलाहाबादी ने यहां गैरलागू अन्य सन्दर्भ में कहा था ‘‘वो ही कातिल, वो ही शाहिद, वो ही मुंसिफ ठहरे। अंगरेजों से उधार लेकर उस पर आचरण करना भारतीय न्यायशास्त्र में पारम्परिक हो गया है। यह कि पीठ पीछे सुनवाई नहीं होनी चाहिए। आरोपी को अपने बचाव का विधिसंगत पूरा मौका मिलना चाहिए। सौ मुलजिम छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा दी गई सजा के बारे में अपील नहीं है। संविधान पीठ तक कई मामले बार बार समझाए जाते या बड़ी पीठ में भेेजे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकार को सलाह भी दी है कि अमुक तरह का कानून बनाने पर सोचे क्योंकि वैसा कानून नहीं होने से न्याय मुकम्मिल तौर पर करने में कठिनाई या असंभाव्यता हो सकती है। अवमानना अधिनियम 1971 मुकम्मिल कानून कतई नहीं है। उसमें खुद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड वरिष्ठ जजों की राय के अनुसार संशोधन की जरूरत है। तब उसकी भी अनदेखी बिना संविधान पीठ में विचारण के क्या हो सकती है?
(7) सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई पूर्व जजों ने इस मामले में अलग अलग कारण (भी) लिखते लेकिन एक दूसरे से सहमत तार्किक सिद्धांत मौजूदा जजों के सामने एकजाई कर भेज दिए हैं। वह फकत बौद्धिक या अकादेमिक बांझ राय नहीं है। वह ‘अन्दरखाने’ के वरिष्ठों की अनुभवजन्य संवैधानिक ‘सलाह’ है। उसका आशय या संकेत यही है कि हमारे वक्त यह मामला आया होता (जो कि आ सकता था, लेकिन नहीं लाया गया) तो हम वैसा ही फैसला करते, जैसी राय अभी दे रहे हैं। इस तरह यह भी यह एक संवैधानिक ऊहापोह की चुनौतीपूर्ण स्थिति है कि न्याय उस वक्त किया जा रहा है, जब बहुत देर हो चुकी है। उस वक्त नहीं किया जा सका जब उसे विचारण में लिया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट प्रशासनिक हैसियत में चूक करे, तो न्यायिक हैसियत में उसका खामियाजा वाचाल और झगड़ालू समझा जाता कर्मठ और असमझौताशील वकील अपनी छाती पर अकेला क्यों झेले?
अवमानना अधिनियम की धारा 20 कहती है ‘‘अवमान के लिए कार्यवाहियां करने की परिसीमा कोई न्यायालय अवमान के लिए कार्यवाहियां, यो तो स्वयं स्वप्रेरणा पर या अन्यथा, उस तारीख को जिसको अवमान का किया जाना अभिकथित है, एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् प्रारम्भ नहीं करेगा।’’ इसका क्या आशय है? सुप्रीम कोर्ट एक वर्ष तक खामोश रहकर अवमानना की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। प्रशांत का मामला पंजीबद्ध होकर ग्यारह साल तक ठंडे बस्ते में रहे। फिर एकाएक मामला गर्म हो जाए। यह मुद्दा भी विचारण मांगता है कि कब तक कोई संशय में रखा जाए। खुद सुप्रीम कोर्ट भुला दे। फिर एकाएक याद करे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों सहित जनमानस ही उद्वेलित हो जाए।
(8) अवमानना अधिनियम की धारा 13 कहती है: ‘‘13. कतिपय मामलों में अवमानों का दंडनीय न होना-तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी-(क) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन न्यायालय अवमान के लिये दंड तब तक अधिरोपित नहीं करेगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि अवमान ऐसी प्रकृति का है कि वह न्याय के सम्यक् उनुक्रम में पर्याप्त हस्तक्षेप करता है, या उसकी प्रवृत्ति पर्याप्त हस्तक्षेप करने की है, (ख) न्यायालय, न्यायालय अवमान के लिए किसी कार्यवाही में, किसी विधिमान्य प्रतिरक्षा के रूप में सत्य द्वारा न्यायानुमत की अनुज्ञा दे सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि वह लोकहित में है और उक्त प्रतिरक्षा का आश्रय लेने के लिए अनुरोध स्वभाविक है।’’
उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि अदालतों द्वारा यक- ब-यक किसी नागरिक की अभिव्यक्ति के खिलाफ अवमानना अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यदि मान लिया है कि प्रशांत भूषण की टिप्पणियां संयत, भद्र, माकूल और तर्कसम्मत नहीं हैं। तो भी क्या विचार हो सकता है कि वे बाद में लगातार मुकदमे लड़ते और कई कथित कटाक्ष भी करते रहे। उनके द्वारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में नागेश्वर राव की नियुक्ति को लेकर गलत तथ्य कहने का आरोप लगाते अटॉर्नी जनरल ने शिकायत भी की थी। प्रशांत भूषण को मिली जानकारी विश्वसनीय नहीं होने से उन्हें उस मामले से पीछे हटना पड़ा था और वह सफाई उन्होंने अटॉर्नी जनरल को दी थी। तब मामला रफा दफा कर दिया गया था। धारा 13 की इबारत के अनुसार क्या प्रशांत भूषण की टिप्पणी जनहित में नहीं है। फिलहाल यह सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। लोकहित तो बहुत खुला हुआ शब्द है। सुप्रीम कोर्ट लोकहित का प्रतिनिधि नहीं है तो क्या निर्धारक हो सकता है? वह तो न्याय करता है। क्या देश के मशहूर विद्वानों, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की राय और सोशल मीडिया पर डाली जा रही टिप्पणियों का आकलन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को फिर भी लगा सकता है कि प्रशांत भूषण ने जनहित के खिलाफ आचरण किया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार बहुत व्यापक और असरकारी होते हैं। इसलिए यदि सुप्रीम कोर्ट से केवल यही अनुरोध किया जा रहा है कि वह तेज गति से चलने के बदले धीमी गति से चले। तो मामले का ऐतिहासिक व्याख्या में निरूपण जरूरी भी हो सकता है। गांधी भी तो कहते थे कि जीवन में धीमी गति जरूरी है जिससे कोई दुर्घटना नहीं हो।
(9) सोशल मीडिया पर विद्वानों की बहार है। अब उन्हें साजिश के तहत इक_ा किया जा रहा है कि वे सबसे बड़ी अदालत की कथित प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए लामबंद होना महसूस करें। अन्यथा वे प्रशांत भूषण के लिए 2009 से खामोशी में बैठे थे। बहुतों को नहीं मालूम होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता की परिभाषा में सुप्रीम कोर्ट अदालत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान निर्मााताओं ने अदालती परिभाषा से ऊपर रखते हुए उसे मूल अधिकारों के परिच्छेद में अनुच्छेद 32 में रखा।’’ 32. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार-(1) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समवेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। (2) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं, जो भी समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी।’’
सुप्रीम कोर्ट भी संसद की तरह कानून बना सकने की गंगोत्री है। उसके अस्तित्व में ही संविधान के मर्म का निचोड़ है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उसका हर फैसला बल्कि कानून देश की सभी अदालतों पर हुक्मनामे की तरह चस्पा हो जाता है। ‘‘141. उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना-उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी।’’ प्रशांत भूषण के मामले का फैसला न्यायिक भविष्य में सभी निचली अदालतें मानने बाध्य होंगी। प्रशांत भूषण की नस्ल और प्रकृति के संविधान जिज्ञासु न जाने कितने अज्ञात वकील और नागरिक इस संभावित फैसले को नज़ीर बनाकर प्रभावित किए जाएंगे। इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों से संविधान का इतिहास और भविष्य भी खुद जिरह कर रहे हैं। वे ऐसे निर्णय की उम्मीद कर रहे हैं जिससे संविधान का चेहरा अंतरराष्ट्रीय इजलास में जगमगाता दिखाई दे।
(10) विश्व के महानतम जजों में एक लॉर्ड डेनिंग के फैसलों से अवगत हुए बिना सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने 1950 के दशक में उसी बिन्दु पर फैसला किया था जो विश्व इतिहास में अमर है। नागरिक आजादी के क्षितिज का सबसे बड़ा विस्तारण 5 जजों की संविधान पीठ के अल्पमत जज हंसराज खन्ना ने किया। वह पूरी दुनिया में संविधान के विद्यार्थियों द्वारा सिर माथे लगाया जाता है। खन्ना आपातकाल के लागू रहते भी अपने न्यायिक ज्ञान की रीढ़ की हड्डी सीधी रख पाए थे। सुप्रीम कोर्ट जवाबदेह प्रजातांत्रिक संस्था है।
हाई कोर्ट के जजों के तिहाई पदों पर उसी हाईकोर्ट के वकील वरिष्ठ जजों के आंतरिक फैसलों के जरिए मनोनीत कर माई लॉर्ड बना दिए जाते हैं। तरक्की पाकर सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाते हैं। यह संकीर्ण आत्मतुष्ट सिद्धांत है। उसे संसद और विधि आयोग ने बदलकर लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे एक अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। हालांकि उसमें खामियां भी थीं। जज बनाने के लिए संविधान कहता है सुप्रीम कोर्ट (या चीफ जस्टिस) से सलाह की जाएगी। ‘सलाह’ शब्द की खुद व्याख्या करते सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उसे ‘सहमति’ समझा जाए। इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्तियों के लिए एक आंतरिक संस्था कॉलेजियम (जिसमें सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठतम पांच जज होंगे) के नाम से खुद बना ली। अब उसकी सहमति लेनी होती है। 2009 से 2014 के दरम्यान सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 50 जज रिटायर हो गए होंगे। उनमें से ही कुछ जज मुखर और तार्किक होकर प्रशांत भूषण के पक्ष में अपने संवैधानिक ज्ञान का लोकव्यापीकरण कर रहे हैं। रिटायर हो जाने से उनकी संवैधानिक समझ की हैसियत की ‘पब्लिक डोमेन’ में आने के बावजूद अनदेखी के लायक हो सकती है? उनके ही पुराने फैसलों को नजीर बनाकर बाद के जज उन बौद्धिक सीढिय़ों पर चढ़ते संवैधानिक व्याख्याओं को तरोताजा बनाए रखते हैं।
(11) किसी साधारण नागरिक की मानहानि हो। तो भारतीय दंड संहिता में कई अपवाद उसे बचाने के लिए हैं।
मसलन यदि वह सच कहता हुआ लांछन लगा रहा हो, या किसी लोकसेवक के आचरण के विषय में सद्भावनापूर्वक कह रहा हो, या परनिंदा कर रहा हो कि वह उस व्यक्ति पर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाए, या अपने या अन्य के हितों की संरक्षा के लिए सद्भावनापूर्वक लांछन लगा रहा हो, या जिस व्यक्ति के खिलाफ कह रहा हो वह लांछन उसे सुधारने या लोककल्याण के लिए हो।
तब वह मानहानि का मामला नहीं ही बनता है। संविधान सभा ने 1949 में और संसद ने 1971 में विधायन करते सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा किया है। इसलिए अदालत की अवमानना के लिए नागरिक अधिकारों की हिफाजत की तरह अपवाद नहीं लिखे। यह इतिहास सुप्रीम कोर्ट के विचारण में रहा है। कोई प्रशांत भूषण बनकर व्यवस्था से उत्पन्न कुछ परिणामों को लेकर उत्तेजित होकर अनर्गल भी कह दे। तो उसे पी. शिवशंकर के प्रकरण में जस्टिस सव्यसाची मुखर्जी या गांधीजी के प्रकरण में अंगरेज जज जस्टिस हेवार्ड की भाषा में अवमाननाकारक नहीं माना गया था। ऐसे साहसी (?) व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट अपनी उदारता में लचीलेपन के साथ व्याख्यायित कर दे। तो उससे तो सुप्रीम कोर्ट का मर्तबा और बढ़ सकता है।
(12) आज न्यायपालिका की देश को पहले से ज्यादा जरूरत है। कार्यपालिका अर्थात मंत्रियों और विधायिका अर्थात (कई गैरजिम्मेदार) विधायकों और सांसदों में से कुछ ने (जिनमें लगभग आधे अपराधी भी कहे जाते हैं) देश का माहौल जहरीला बना दिया है। जनता सुप्रीम कोर्ट की ओर लगातार टकटकी लगाकर देखती रहती है। जनता हताश भीड़ नहीं है। वह महान जनसैलाब से है जिसकी कुर्बानियों के कारण भारत को आज़ादी मिली। उसी जनसंकुल के प्रतिनिधियों ने खुद सुप्रीम कोर्ट की राय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा 90 हजार शब्दों का संविधान रचा। किसी को भी नायक या खलनायक बनाने का सवाल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अंतरराष्ट्रीय अहमियत, प्रसिद्धि और स्वीकार्यता होने से ही भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सिरमौर बन सकेगा। यही हर विवेकशील नागरिक के विवेक की कशिश है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की कलमें न्याय के क्षेत्र में इतिहास भी लिखती हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने नेहरू, अंबेडकर और राजेन्द्र प्रसाद की अगुवाई में खास चरित्र के विवेक की उसमें रोशनाई भरी है। वह विवेक प्रकारांतर से जनता के खून, पसीने और आंसू बहाने के बाद के संघर्ष से उपजा था। प्रशांत भूषण का मामला केवल पक्षकारों का विवाद नहीं है। प्रशांत भूषण को तो इतिहास ने अब अवसर दे दिया है कि वे जनअपेक्षाओं के प्रतीक, प्रवक्ता या प्रस्तोता बनकर सुप्रीम कोर्ट के सामने संविधान निर्माताओं और व्याख्याताओं की जिरह को विन्यस्त, विकसित और विस्तारित करें। सुप्रीम कोर्ट के जजों के सम्मान, स्वाभिमान और स्वविवेक की रक्षा तथा संस्था की हिफाजत करना हर नागरिक का संवैधानिक और लोकतांत्रिक कर्तव्य है। अज्ञान, हताशा अतिरिक्त आत्मविश्वास और नासमझी के कारण सोशल मीडिया पर टिप्पणियां होती रहती हैं। उन्हें संविधान रामायण के मूल पाठ की चैपाई, दोहा या सोरठा नहीं समझा जाना चाहिए। वे ज्यादा से ज्यादा क्षेपक हैं। यह लेख भी एक क्षेपक है। इसमें मुझ अभिव्यक्तिकार की पीड़ा, जिज्ञासा, परेशानदिमागी और उत्कंठा है। इसमें पूर्वग्रह, खीझ, आक्रोश, अविश्वास या नासमझी की ऊहापोह नहीं है। देखें! भारत की जनता संविधान निर्मााता के रूप में अपना खुद का भविष्य आने वाले इतिहास के बियाबान में किस तरह बांचती है।
(13) यूरो-अमेरिकी मॉडल के संविधान से लिए गए अधिकारों के बचाव के लिए संविधान सलाहकार बी.एन. राव, अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश फेलिक्स फ्रैंकफर्टर से मिले। उनकी सलाह पर नागरिक आजादी और अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध रचे गए। मूल अधिकारों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल ने रिपोर्ट सौंपते कहा था यदि मूल अधिकार छीने जाएं तो अदालतें हस्तक्षेप करेंगी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था अदालतों को पूरी आजादी दे देने से सुप्रीम कोर्ट को विधायिका की मर्यादा और कार्यपालिका की जवाबदेही तय करने के अधिकार दिए गए तो सुप्रीम कोर्ट अमेरिकन थ्योरी के तहत, पुलिस अधिकारों के तहत शक्तियों की मीमांसा कर सकता है। नागरिक आजादी पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद हम बार बार डींग मारते हैं कि भारत का संविधान दुनिया के सबसे उदार संविधानों में एक है। संविधान सभा में महबूब अली बेग ने बताया कि अलबत्ता ऐसे प्रतिबंध जर्मनी के संविधान में हैं। तानाषाह हिटलर चाहता था ऐसे कानून बनें जिनका विरोध तक नहीं किया जा सके। स्वतंत्र बुद्धि के अंगरेज पत्रकार बी.जी. हार्निमेन और महात्मा गांधी के बेटे देवदास गांधी को भी अपने अखबारों में अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करने के कारण अदालती अवमानना के नाम पर जेल की सजा हुई थी। अवमानना का प्रतिबंध फिर भी संविधान की आंत में ठहर गया।
(14) सुप्रीम कोर्ट में जब बहुत जटिल संवैधानिक जिरह होती है, तो पांच या अधिक जजों की संविधान पीठ बनाने का नियम और परंपरा है। सुप्रीम कोर्ट में आज तक के सबसे बड़े मुकदमे केशवानन्द भारती में संविधान का बुनियादी ढांचा क्या है, पर फैसला 7 बनाम 6 के बहुमत से हुआ। अल्पमत के 6 जजों की समझ का इतिहास में क्या लब्बोलुबाब बनेगा? टी.एम. ए पाई फाउंडेशन के 11 सदस्यीय बेंच के फैसले ने क्या कहा, उसे। बाद में 5 जजों की इस्लामिक एजुकेशन सोसायटी वाली बेंच ने समझाया। फिर दूसरी बेंच के खिलाफ भी 7 जजों की पी. ए. इनामदार के मामले वाली तीसरी बेंच ने समझाया। अटपटी भाषा में लिखे फैसलों को खुद सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज तक समझ नहीं पाते। तब बार बार उन्हें तर्क की सान पर खुद चढ़ाते हैं। प्रशांत भूषण के कारण हर नागरिक की अदालत की आलोचना करने के अधिकार पर बंदिश लगने के खतरे भी कुलबुला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को हर तरह के आरोप, दुराचरण और छींटाकशी से मुक्त रखना भी संविधान का आग्रह है। हर नागरिक की अभिव्यक्ति की आजादी की पतंग आसमान में जितनी ऊंचाई तक चाहे उड़ाई जा सकती है। उसकी डोर अंतत: सुप्रीम कोर्ट के हाथ होती है। उड़ती तो वही है जो उड़े, कटे नहीं। आसमान तक उडऩा ही तो नागरिक अभिव्यक्तियों का लक्ष्य होता है।
(15) मशहूर संविधानविद एस.पी. साठे अपनी पुस्तक में सवाल उठाते हैं ‘‘क्या अवमानना के कानून को सामाजिक सक्रिय संगठनों द्वारा की जा रही आलोचना के लिए ज्यादा सहिष्णुता प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए?’’ एक महत्वपूर्ण जज चिनप्पा रेड्डी ने फैसले को असंगत, गैरतार्किक और अरुंधति की पीड़ा समझने में असमर्थ करार दिया है। बाबरी मस्जिद को बचाने का झूठा हलफनामा देकर मस्जिद का ढांचा गिर जाने पर भी तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अवमानना प्रकरण में 28 साल बाद भी चुप्पी है। कई प्रबुद्ध व्यक्ति सच कहना चाहते हैं लेकिन अवमानना कानून के पसरते हुए डैनों के डर के कारण संभव नहीं होता। इसलिए सुप्रीमकोर्ट के वे फैसले महत्वपूर्ण हैं जहां संविधान और कानून के जानकारों तथा उस प्रक्रिया में संलग्न विधि विशेषज्ञों द्वारा कभी उत्साह में भी कर दी जाती रही टिप्पणियों पर उदार और सजारहित लोकतांत्रिक फैसले हुए हैं।
(16) सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनहित में न्याय करने का एक और पक्ष है। (संभवत) जस्टिस पी. एन. भगवती ने साधारण नागरिकों से प्राप्त चिट्ठियों को जनहित याचिकाओं में बदलकर अथवा अखबारों के समाचार पढक़र संविधान न्यायालय के मुताबिक न्याय देने की कोशिश करने की पहल की थी। उसे कई जजों ने लगातार कायम रखा। भले ही मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने एक अनुदार संकोच ओढ़ लिया है।
एक दिलचस्प मोड़ तो इस तरह भी आ सकता था कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चार जज रोहिंग्टन, नरीमन, उदय ललित, एन. नागेश्वर राव और इंदु महोत्रा वर्षों से प्रशांत भूषण के सुप्रीम कोर्ट बार में साथी वकील रहे हैं। यदि इनमें से से बेंच बनती तो मामले में कई ऐसे तथ्य भी आते अथवा बहस होती जो पुरानी घटनाओं के सिलसिले में उनके पास पुष्ट सूचनाओं के रूप में उपलब्ध समझे जा सकते हैं। जस्टिस नरीमन, उदय ललित तथा प्रशांत भूषण के पिता सुप्रीम कोर्ट के बहुत वरिष्ठ वकीलों में गिने जाते हैं। हालांकि यह केवल एक मनोविलास का तर्क है। सुप्रीम कोर्ट तो सार्वभौम है।
देश के कई हाई कोर्ट में नए नए बने जज भी सैकड़ों की संख्या में पक्षकारेां को और कुछ वकीलों को भी अवमानना नोटिस देते रहते हैं। भले ही तीन चौथाई मुकदमों में बस केवल माफीनामा दे देते हैं। ऐसे में इस बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान का बहुत लोकधर्मी चलन भी तो होना मुनासिब नहीं लगता। संभवत: सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे आंकड़े मंगाकर उस पर कभी विचार किया हो। विधि आयोग की भी अपनी सिफारिशें रही हैं। कुल मिलाकर यह जरूरी है कि न्याय किया जाने पर भी उससे जुड़ी परिस्थितियों और परिणामों के सिलसिले में उसे बहस के लिए न्याय्य (जस्टिशिएबल) बनाया जाना भी संविधान का मकसद, आग्रह और आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में बिना किसी पूर्वग्रह के उसकी गरिमा की रक्षा करना संसद, सरकार, वकीलों, जनता, मीडिया और खुद सुप्रीम कोर्ट का संविधान के प्रति अर्थात जनता के प्रति बुनियादी कर्तव्य है।





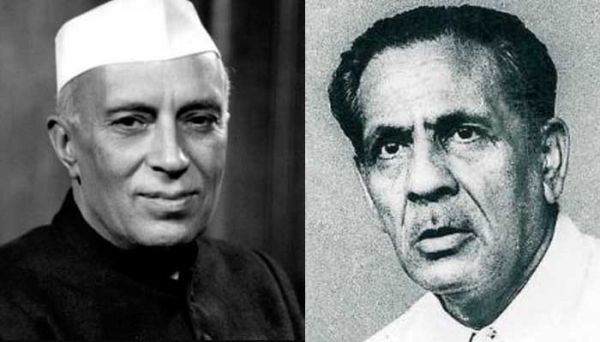
.jpg)