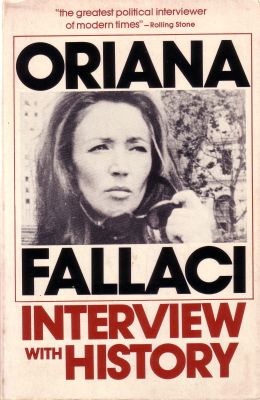विचार / लेख

-दिनेश श्रीनेत
जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक में लाइव का फीचर जोड़ा गया तो ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल जीवन की हलचल या किसी इवेंट की झलक दिखाने के लिए करते थे। कोई अपने बच्चों की शरारतें लाइव करता था तो कोई संगीत का प्रोग्राम। किसी ने यह नहीं सोचा था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ किसी के विचार सुनने या बहस या संवाद के रूप में भी हो सकता है।
कोरोना काल में जब न कॉफी हाउस रहे, न ऑ़़डिटोरियम और न ही छोटी-मोटी सभाओं की गुंजाइश रही तो आनन-फानन में बहुत से लोगों ने इस माध्यम का प्रयोग किया और इसे साधते चले गए। बाकी भाषाओं का मुझे नहीं पता मगर हिंदी साहित्य ने तो इस माध्यम के जरिए अपनी वैचारिकी गढ़नी आरंभ कर दी है।
हिंदी के शीर्षस्थ आलोचक नामवर सिंह ने बहुत पहले ही सीधे संवाद माध्यम की ताकत को पहचाना और लिखने की बजाय बोलने की राह चुकी। यह हमारा दुर्भाग्य है कि जिस दौर में उन्होंने यह करना आरंभ किया था, हमारे पास डाक्यूमेंटेशन के तरीके बहुत कम और खर्चीले थे। बीते दौर के साहित्यकारों को लाइव सुनने के लिए हमारे पास दूरदर्शन के प्रोग्राम और कुछ डाक्यूमेंट्रीज़ भर हैं।
मुझे निजी तौर पर ऐसा लगता है कि छपे हुए शब्दों के विस्तार की अपनी सीमाएं हैं। हिंदी में साहित्यिक पत्रिकाएं निकालना न सिर्फ खर्चीला है बल्कि उसकी प्रसार संख्या भी बहुत सीमित है। कुछ पत्रिकाओं को छोड़ दें तो बाकी लघु पत्रिकाओं की स्थिति पुराने समय में निकलने वाली स्मारिकाओं जैसी रह गई है, जिसे जान-पहचान वालों के बीच बांटकर खपाना पड़ता है। वहीं डिजिटल ने बड़ी संख्या में हिंदी के पाठक तैयार किए हैं। उन पाठकों में नई सूचनाओं की भूख है। वे नए विषयों और मुद्दों को जानना-समझना चाहते हैं।
खुद अपनी प्रोफायल से किए गए किसी भी ठीक-ठाक फेसबुक लाइव में औसत उपस्थिति 25 से 50 के बीच होती है और बाद में उसे देखने वालों की संख्या औसतन एक हजार से 5-6 हजार तक पहुँच जाती है। इस मुकाबले में साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रसार बहुत कम होता है। दूसरे, इनमें जो कुछ भी छपता है अब हिंदी समाज के पास ऐसे ठिकाने बहुत कम रह गए हैं जहां इन पर चर्चा हो सके। पुराने कॉफी हाउस या तो बंद हो गए या वहां सन्नाटा पसरा रहता है। साहित्यिक गोष्ठियों में या वक्ता ही श्रोता होते हैं या जबरन डमी दर्शकों को बिठाया जाता है।
इसके अपवाद हैं मगर दिल्ली जैसी जगहों पर भी ऐसे अपवाद साल में आठ-दस बार घटित होते हैं जबकि साहित्यिक और वैचारिक आयोजन हफ्ते में आठ-दस होते हैं। फेसबुक लाइव की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वहां सुनने वाले को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आजादी होती है, जबकि परंपरागत साहित्यिक आयोजनों में माहौल शादी-ब्याह जैसा होता है, जहां लोग बधाई देते या आयोजन के मूल विषय से इतर चर्चा करते नजर आते हैं। कुछ लोग 20 मिनट बैठने के बाद बाहर चले जाते हैं और चाय-कॉफी के साथ अपनी नेटवर्किंग में व्यस्त हो जाते हैं। वहीं डिजिटल आयोजनों में वही चेहरे दिखते हैं जिनकी दिलचस्पी विषय में होती है।
यहां एक बात और भी गौर करने लायक है। कितना भी बड़ा या चर्चित नाम क्यों न हो अगर वो काम की बात नहीं कर रहा है तो उसके लाइव में कम लोग ही दिखते हैं। वहीं कई युवा चेहरों ने डिजिटल में अपार लोकप्रियता बटोरी है। असहमति में यह तर्क भी दिया जाता है कि साहित्यिक पत्रिकाओं की अपनी एक स्तरीयता है। इसमें कोई संदेह नहीं मगर यह भी उतना कड़वा सच है कि हंस व पहल जैसी पत्रिकाओं को छोड़ दें तो ऐसी पत्रिकाएं साहित्य में केंद्रीय भूमिका से हाशिये की तरफ खिसकती जा रही हैं। हर पत्रिका का अपना क्षेत्र है, अपने लेखक हैं और अपना एक ग्रुप है जहां पर उसका वितरण होता है।
इस लिहाज से मुझे डिजिटल ज्यादा व्यापक और उदार माध्यम लगता है। ऑनलाइन साहित्यिक पत्रिकाओं ने अपनी कोई ख्याति नहीं दर्ज की। इसकी एक वजह यह रही कि बहुत से गंभीर साहित्यकारों ने इस माध्यम से परहेज बनाए रखा और बहुत सी पत्रिकाओं के संचालकों ने लोकप्रियता और परिचय के लालच में औसत रचनाओं को भी खूब छापा। बेहतर ऑनलाइन साहित्यिक पत्रिका निकालना भी एक कला है, जिसे फिलहाल मौजूदा संचालक नहीं साध पाए हैं। कहीं कंटेंट अच्छा है तो तकनीकी स्तर पर बहुत खराब हैं और कहीं बाकी बातों का ध्यान रखा गया है तो कंटेट पर फोकस नहीं है।
रेख्ता, हिन्दवी, हिंदीनामा, सदानीरा जैसे प्लेटफॉर्म इसी बीच सामने आए। पिछले दिनों राजकमल ने व्हाट्सऐप के माध्यम डिजिटल पत्रिका का जो प्रयोग किया उसमें बड़ी संभावनाएं हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा बड़ी संभावनाओं वाला माध्यम वह है जिसका जिक्र मैंने आरंभ में किया। रचनाकार और पाठक का सीधा संवाद। सीधे कविताएं और कहानियां सुनना, सीधी चर्चा में भाग लेना, विचारों को सुनना- इसका एक अलग सुख और संभावनाएं हैं। इसने हमारी हिंदी की वैचारिकी में एक नया आयाम जोड़ा है।
भारतीय परंपराओं में सीधे संवाद का बड़ा योगदान है। पुरा-काल में सारा ज्ञान इन्हीं संवादों का नतीजा था। यह समाज लिखने, लिख हुए को गुनने और उस पर जवाब लिखने वाला समाज नहीं है। वह पश्चिम में था। जिसकी वैचारिकी का सीधा संबंध छापाखाने के अविष्कार और प्रसार से था। यह समाज बोलने, सुनने और सुने पर चर्चा करने वालों का समाज है। नई तकनीकी ने खोई हुई इस परंपरा को दोबारा हासिल करने में मदद की है।
यह सब कुछ संभव हुआ है इसी कोरोना काल में और इसमें कोई संदेह नहीं कि इसने एक नई दुनिया के दरवाजे खोले हैं। प्रायोजित गोष्ठियों, आत्ममुग्ध वार्तालापों और सीमित दायरे के संवादों से अलग यहां विचारों का दस्तावेजीकरण भी संभव हुआ है, कही गई बातें अब रिकॉर्ड में हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि यह माध्यम उत्तर-कोरोना काल में धुमिल नहीं होगा और हिंदी में वैचारिकी एक नए तरीके से विस्तार लेगी। (फेसबुक से)