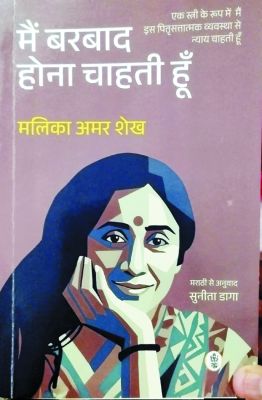विचार / लेख

-चित्रगुप्त
1724 का वह काला अध्याय इतिहास में दर्ज है, जब पश्चिम अफ्रीका के घने जंगलों से मात्र चौदह वर्षीय थॉमस फुलर को गुलाम बनाने वाले अपहरणकर्ता बेडिय़ों में जकडक़र अमरीका ले आए। औपनिवेशिक वर्जीनिया की ज़मीन पर उतरा यह बच्चा न पढऩा जानता था, न लिखना। लेकिन उसके दिमाग में जो था, वह किसी भी सभ्य समाज की कल्पना से कहीं आगे था। गुलामी की जंजीरों के भीतर बंद यह किशोर एक चलता-फिरता गणित था। इसलिए लोग उसे ‘वर्जीनिया कैलकुलेटर’ कहने लगे।
1780 के दशक में जब दो शिक्षित क्वेकर सज्जन-विलियम हार्टशॉर्न और सैमुअल कोट्स—ने उसकी परीक्षा ली, तो सभ्यता खुद कटघरे में खड़ी हो गई। डेढ़ साल में कितने सेकंड होते हैं-थॉमस ने बिना कागज़़-कलम, एक मिनट से कम में सही उत्तर दे दिया। 70 साल, 17 दिन और 12 घंटे में कितने सेकंड-यह भी उसने लगभग डेढ़ मिनट में गिन दिया। जब शिक्षित व्यक्ति ने उत्तर को ग़लत बताया, तो गुलाम लडक़े ने शांति से कहा-आप लीप ईयर भूल गए हैं। दोबारा गणना हुई, और वही सच निकला जो एक अनपढ़ गुलाम ने कहा था।
यह घटना इसलिए दर्ज हुई क्योंकि इसे डॉ. बेंजामिन रश जैसे प्रतिष्ठित विद्वान ने लिखा। नहीं तो इतिहास अक्सर ऐसी प्रतिभाओं को चुपचाप दफऩा देता है। थॉमस फुलर 1790 में मर गया, लेकिन वह यह सवाल छोड़ गया कि अगर बुद्धि रंग, नस्ल, शिक्षा या हैसियत की मोहताज नहीं है, तो इंसानी समाज उसे इन जंजीरों में क्यों बाँधता है?
यूरोप और अमरीका ने लंबे समय तक नस्ल के नाम पर यह झूठ फैलाया कि कुछ लोग जन्म से ही श्रेष्ठ होते हैं और कुछ जन्म से ही हीन। थॉमस फुलर जैसी कहानियाँ उस झूठ को तार-तार कर देती हैं। यह बताती हैं कि प्रतिभा प्राकृतिक होती है, सामाजिक नहीं। वह किसी चमड़ी, किसी कुल, किसी धर्म या किसी दर्जे से नहीं निकलती—वह इंसान से निकलती है।
लेकिन अगर हम यह सोचते हैं कि नस्ल का यह ज़हर सिफऱ् पश्चिमी इतिहास की बीमारी थी, तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं। भारत में यही धारणा जाति व्यवस्था के रूप में आज भी जि़ंदा है। यहाँ भी जन्म के आधार पर यह तय करने की कोशिश होती है कि कौन तेज होगा, कौन योग्य होगा, और कौन सिर्फ ‘आरक्षण का लाभार्थी’ कहलाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ गुलामी की जंजीरें दिखाई नहीं देतीं—वे अंकतालिकाओं, इंटरनल असेसमेंट, मौखिक परीक्षाओं और ‘मेरिट’ के दावों में छुपी होती हैं।
इसी संदर्भ में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल और उसके मेडिकल कॉलेज का वह मामला याद किया जाना चाहिए, जहाँ वर्षों तक एक ही विषय में वही छात्र बार-बार फेल होते रहे। जाँच हुई तो आरोप सामने आए कि उत्तर पुस्तिकाएँ पहचानकर देखी गईं, और दलित-आदिवासी छात्रों को व्यवस्थित ढंग से फेल किया गया। यह कोई सडक़-छाप संस्थान नहीं था, बल्कि देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक था। यानी जहाँ देश के डॉक्टर बनते हैं, वहीं जाति यह तय कर रही थी कि कौन डॉक्टर बनने लायक है और कौन नहीं।
यहाँ सवाल सिर्फ कुछ छात्रों के फेल होने का नहीं है। सवाल उस मानसिकता का है जो यह मानकर चलती है कि कुछ लोग थॉमस फुलर हो ही नहीं सकते—कि उनकी प्रतिभा संदिग्ध है, कि उन्हें ज़्यादा कड़ी परीक्षा से गुजऱना चाहिए, कि उनका पास होना अपने-आप में शक पैदा करता है। यह वही मानसिकता है जिसने कभी अश्वेत गुलाम को ‘कम अक्ल’ कहा था, और आज दलित छात्र को ‘कम मेरिट’ वाला कहती है।
थॉमस फुलर की कहानी इसलिए आज भी ज़रूरी है, क्योंकि वह सिर्फ इतिहास नहीं है—वह आईना है। वह हमें दिखाती है कि समाज बार-बार प्रतिभा को पहचानने में नहीं, उसे स्वीकार करने में चूक करता है। चाहे वह अठारहवीं सदी का अमरीका हो, या इक्कीसवीं सदी का भारत—जब भी इंसान ने बुद्धि को जन्म से बाँधने की कोशिश की है, उसने खुद को छोटा किया है।
नस्ल हो या जाति, दोनों एक ही झूठ के अलग-अलग नाम हैं। और थॉमस फुलर जैसे लोग उस झूठ के खिलाफ सबसे मजबूत सबूत हैं-एक ऐसा सबूत, जिसे न इतिहास मिटा सका, न सत्ता, न व्यवस्था।(यह लेख संपादक सुनील कुमार के तर्कों पर, उनके बताए मुताबिक chatgpt ने लिखा है).