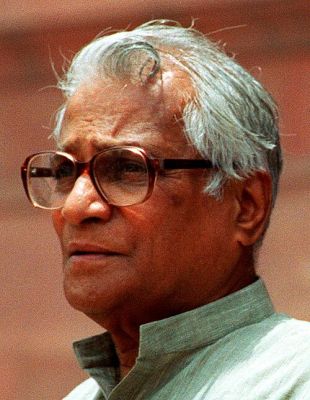विचार / लेख
- श्रुति व्यास
हम खतरनाक समय में जी रहे हैं! और यह न रूपक में, न मनोदशा में, बल्कि मापी जा सकने वाली सच्ची बात है। यह किसी हेडलाइन या चिंता से उपजी अतिशयोक्ति नहीं है। यह विज्ञान है। मानवता अब आत्मविनाश के कितने करीब पहुँच चुकी है, इसका प्रतीक ‘डूम्सडे क्लॉक’ का इस साल 89 सेकंड पर टिकना है, आधी रात के, यानी विनाश के, सबसे नजदीक।
‘बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स’ के वैज्ञानिकों और नोबेल विजेताओं की समिति ने यह समय इस साल आगे बढ़ाया, इस चेतावनी के साथ कि दुनिया अब परमाणु दुस्साहस, जलवायु अराजकता, तकनीकी अतिरेक और भ्रामक सूचनाओं के दलदल में डूब रही है।
उनके शब्दों में- ‘हम वैश्विक तबाही की ओर बढ़ रहे हैं-रूपक रूप में नहीं, बल्कि नापने योग्य रूप में।’ और यह सब दिखता है। मौसम पागल हो चुका है। इस साल भारत ने ही काफी तबाही झेली, पहाड़ काँपने लगे हैं, नदियाँ विद्रोह कर रही हैं, और शहर अपनी ही महत्वाकांक्षा में घुट रहे हैं।
धरती को इतना खोदा जा चुका है कि ज़मीन अब खोखली महसूस होती है। यहाँ तक कि आसमान भी बदल गया है अब वह शांत, दार्शनिक नीला नहीं जो कभी हमें ठहरकर ऊपर देखने को मजबूर करता था। वह नीला अब जलता है, धुंध और ताप से धुँधला हुआ, जैसे क्षितिज पर खुद प्रकृति ने चेतावनी लिख दी हो।
लेकिन पतन सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, वह राजनीतिक भी है और डरावनी बात यह है कि वह लोकतांत्रिक भी है। आज दुनिया की अव्यवस्था केवल तानाशाहों की बनाई नहीं है, उसे लोकतंत्रों ने भी मिलकर गढ़ा है, और शायद परिष्कृत भी किया है। जो देश कभी अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के स्थापक थे, वे अब अपने ही घरों में उसे तोड़ रहे हैं। वे संस्थाएँ, जो सत्ता के अतिरेक से नागरिकों की रक्षा के लिए बनी थीं-संसदें, अदालतें, मीडिया, विश्वविद्यालय-वे सब राजनीतिक दबाव या जन-थकान के बोझ तले चरमराने लगी हैं। लोकतंत्रों के पुराने checks and balances अब संतुलन नहीं बनाते।
वॉशिंगटन में, शासन पार्टीगत नाटक बन गया है। नई दिल्ली में, असहमति को देशद्रोह समझ लिया जाता है। यरूशलम में, न्यायपालिका एक व्यक्ति की इच्छा के आगे झुक जाती है। हमारे समय की अव्यवस्था अब सिफऱ् वैश्विक नहीं, संस्थागत भी है, प्रणालीगत और आत्मनिर्मित। जो शुरुआत लोकतंत्र के क्षरण से हुई थी, वह अब उसके नए रूप में कठोर हो चुकी है- performative populism यानी प्रदर्शनकारी जनवाद। अब सत्ता चुपचाप नहीं चलाई जाती, उसे रोज़ मंचित किया जाता है टीवी पर, सोशल मीडिया पर, रैलियों में। और जो संस्थाएँ सवाल उठाने के लिए बनी थीं, उन्हें हास्यास्पद बनाकर अप्रासंगिक किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की अनदेखी की जाती है, अंतरराष्ट्रीय संधियाँ कमजोर कर दी गई हैं, और मानवाधिकार अब केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं।
जो व्यवस्था के रक्षक थे, वही अब उसे अस्थिर करने वाले बन गए हैं, शक्ति और सुविधा की भाषा में क़ानून को फिर से लिखा जा रहा है।
इस बीच, महाद्वीपों के पार 110 सशस्त्र संघर्ष चल रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा। सिफऱ् एशिया में ही 21 युद्ध सक्रिय हैं, भारत और पाकिस्तान की पुरानी वैर-दृष्टि, भारत और चीन की जमी हुई सीमाएँ, पाकिस्तान और अफग़़ानिस्तान का नया तनाव। ये दूर की जंगें नहीं हैं, यह पड़ोसियों के बीच की लड़ाइयाँ हैं, नदियों, सीमाओं, गर्व और स्मृति के नाम पर।
1990 के दशक का जो ‘शांति लाभांश’ था, वह अब पूरी तरह उड़ चुका है। युद्ध फिर लौट आया है भाषा बनकर, नीति बनकर, विचारधारा बनकर। यहाँ तक कि यूरोप, जिसने दावा किया था कि उसने अपने युद्धों को बीसवीं सदी के मलबे के नीचे दफना दिया है, अब फिर लहूलुहान है। रूस का यूक्रेन पर आक्रमण उस भ्रम को तोड़ चुका है कि ‘युद्ध अब इतिहास हैं।’ और पश्चिम एशिया तो मानो हमेशा जलता रहता है-गाजा, लेबनान, ईरान, यमन-एक संघर्ष पर दूसरा संघर्ष, जब तक विनाश सामान्य नहीं लगने लगता।
हर मोर्चा दूसरे को ईंधन देता है। हर युद्धविराम एक intermission जैसा लगता है, अंत नहीं।
और इस अराजकता के बीच मंच पर आते हैं वे पुरुष-डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, बेंजामिन नेतन्याहू, व्लादिमीर पुतिन, रेचेप तैयप एर्दोगन और उनके जैसे बाकी सब। हर कोई अपने-अपने तूफ़ान का उत्पाद है, पर मिलकर वे शक्ति का एक पैटर्न रचते हैं। वे व्यवस्था को शांत करने नहीं, नियंत्रित करने आते हैं। संस्थाएँ पुनर्निर्मित करने नहीं, उन्हें अपने प्रतिबिंब में ढालने। वे सब एक ही कोरियोग्राफ़ी में चलते हैं, यह भ्रम कि अव्यवस्था को करिश्मे से संचालित किया जा सकता है, कि कानून लोचदार है, और व्यवस्था उसी की है जो उसे फिर से परिभाषित करने का साहस रखता है। उनका उभार राष्ट्रों की ताकत नहीं, नागरिकों की थकान का प्रमाण है, ऐसी जनता की, जो अस्थिरता से इतनी थक चुकी है कि वर्चस्व को ही नियति मान बैठी है। हमारे समय की त्रासदी यही है, पुराने नियम अब लागू नहीं, और कोई उनके लौटने को लेकर nostaligic भी नहीं। 1945 के बाद जो व्यवस्था नैतिक पुनर्निर्माण के आधार पर बनी थी, उसका भार अब खत्म हो चुका है। हम अब ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ नैतिक ज्यामिति नहीं, बल्कि एल्गोरिद्म का हिसाब चलता है। जहाँ आक्रोश भी प्रतिस्पर्धा है, और स्मृति हर न्यूज़ साइकिल के साथ रीसेट हो जाती है।
बीसवीं सदी में दानव थे, लेकिन अपराधबोध भी था। इक्कीसवीं सदी ने तमाशे को पूर्णता दी है। और फिर भी, इतिहास घूमकर वहीं आ गया है। जिस सदी को डिजिटल और लोकतांत्रिक होना था, वह अब मध्यकालीन लगती है, असमानताओं में सामंती, राजनीति में सांप्रदायिक, और नेतृत्व में निरंकुश। दुनिया का नक्शा प्रगति से ज़्यादा पतन जैसा दिखता है, सीमाएँ कठोर, पड़ोसी शत्रु, और राष्ट्र धर्म, पहचान, और भय को हथियार बनाते हुए।
इतिहास बताता है कि लगभग हर बड़ा युद्ध पड़ोसियों के बीच लड़ा गया। हम फिर उसी खतरनाक नजदीकी में पहुँच चुके हैं। इस युग का सबसे बड़ा खतरा युद्धों की संख्या नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारी सहजता है। कभी कहा गया था दुनिया का अंत धमाके से नहीं, फुसफुसाहट से होगा। लेकिन अब शायद यह अंत अलग होगा खामोशी से नहीं, शोर से।
उस शोर से जो क्रोध का है, पर कर्म का नहीं; जो शक्ति का है, पर सिद्धांत का नहीं; उन नेताओं का, जो वर्चस्व को नियति समझ बैठे हैं। डूम्सडे क्लॉक इसलिए अब सिर्फ वैज्ञानिक चेतावनी नहीं, बल्कि मानवीय अहंकार का प्रतीक है। आज यह घड़ी आधी रात से 89 सेकंड दूर है। कल इसकी सुइयाँ फिर चलेंगी-आगे या पीछे-यह इस पर निर्भर करेगा कि हम क्या चुनते हैं- सत्य या प्रचार, संयम या प्रदर्शन, मानवता या अहंकार। क्योंकि हमारा संकट समय का नहीं है, वह बुद्धि का है। (नया इंडिया)