विचार / लेख
-संजय श्रमण
यूरोप में दो भारतीय मिलते हैं तो इंगलिश में बातें करते हैं। दोनों को पता हो कि अगला/अगली हिन्दी बेल्ट से है फिर भी इंगलिश में ही बातें करते हैं। तमिल, तेलुगू या मलयाली भारतीय हों तो बात अलग है लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, हिन्दी बेल्ट का आदमी हिन्दी नहीं बोलना चाहता।
परदेस में दो बंगाली मिलेंगे तो बांग्ला में बोलेंगे, दो तमिल या मलयाली पंजाबी मिलेंगे तो तमिल या मलयालम या पंजाबी में ही बातें करेंगे। इस बात का हिन्दी भाषी बड़ा मजाक बनाते हैं। हिन्दी बेल्ट वाले ना केवल इंगलिश पर आ जाते हैं बल्कि एक्सेंट भी मारने लगते हैं।
यूरोपीय या अमेरिकन लोगों से बात करने के लिए एक्सेंट ठीक है, लेकिन दो भारतीय हिन्दी भाषी एकदूसरे को एक्सेंट में काहे को बतियाते होंगे?
यहाँ एक और मज़ेदार बात है, पाकिस्तानी मित्र मिलें तो एकदम से उर्दू-हिन्दी शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर में हिन्दी उर्दू में हल्की फुलकी शायरी और गालियों तक आ जाते हैं। जब किसी मुद्दे पर अपने अपने नेताओं और मुल्क की बदहाली पर जी भर के उर्दू हिन्दी पंजाबी में गालियाँ दे देते हैं तो बड़ा भाईचारा बन जाता है। फिर इंगलिश में कभी बात नहीं होती।
लेकिन उफ्फ़़! हिन्दी बेल्ट के भारतीयों से परदेस में मिलना उतना अपनापन नहीं देता।
क्या कारण हो सकता है?
मैंने कई लोगों से पूछा, ख़ासकर यूरोपीय विश्वविद्यालयों में कई लोगों से इस विषय में बात की। वे कहते हैं कि भारतीयों में और कुछ अफ्रीकी देशों में ये बात बहुत ज़्यादा है। जहां भी उपनिवेशी क़ब्ज़ा रहा है, वहाँ अपनी भाषा के प्रति एक हीन भावना प्रवेश कर गई है।
भारत में अन्य भाषाओं की तुलना में हिन्दी भाषियों में ये हीन भावना कुछ अधिक है। एक कारण तो ये कि हिन्दी बहुत ही नयी भाषा है। हिन्दी भाषी भारतीय आपस में भी, अपने बच्चों से भी इंगलिश में ही बातें करते हैं। यही हिन्दी-उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानियों के बारे में भी है। इस पूरे ख़ित्ते में जहां भी हिन्दी का असर है, वहाँ अपनी भाषा के प्रति एक ख़ास हीन भावना है।
स्विट्जऱलैंड का आधा हिस्सा जर्मन प्रभाव में है और शेष आधा फ्ऱेंच प्रभाव में है। ये मोटा मोटा विभाजन है। ना इटली में न स्विट्जऱलैंड में इंगलिश बोलने को ज्ञान की या शिक्षित होने की निशानी माना जाता है। जर्मनी और फ्ऱांस में तो कतई इंगलिश की धौंस नहीं जमाई जा सकती। वे लोग जर्मन और फ्ऱेंच के आगे किसी भाषा को कुछ नहीं समझते। ब्रिटेन की तो राजभाषा भी लंबे समय तक फ्ऱेंच ही थी। ये बात कम ही लोग जानते हैं। भारत पर फिर से आते हैं।
भारतीयों में विशेष तौर पर हिन्दी भाषियों में ना जाने कब ये प्रवृत्ति घुस गई कि गऱीब किसानों, मज़दूरों, शिल्पकारों, मछुआरों, चरवाहों के शब्द मानक हिन्दी में शामिल नहीं करने हैं। शास्त्रीयता, शुद्धता, संस्कृतनिष्ठता इत्यादि ना जाने कितने तरह के आग्रह हैं जिनकी वजह से हिन्दी अपने ही देश में अपने ही लोगों में धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है। सामान्य बोलचाल की हिन्दी में जीतने शब्द हैं वे लाखों की संख्या में हैं, लेकिन मानक हिन्दी में शब्द कम होते जाते हैं।
किसानों, मज़दूरों और ख़ास तौर से गाँव के गऱीबों से या झुग्गी झोपड़ी के मज़दूरों से बात करके देखिए, आपको कई नये शब्द मिलेंगे। उदाहरण के लिए ‘गरियाना’ ‘लतियाना’ ‘वाट’ ‘मूड’ ‘ख़ालिस’ ‘ख़लास’ ‘जुगाड़’ ‘खटारा’ ‘भंगार’ और ना जाने क्या क्या। ये सब उनकी हिन्दी में हैं लेकिन किताबी हिन्दी में ये नहीं आ रहे। किताबी हिन्दी में ऐसे शब्द मिलेंगे जो मु_ी भर लोगों को ही समझ में आ सकते हैं।
इसीलिए हिन्दी की किताबें अगर पाँच सौ भी बिक जाये तो चमत्कार हो जाता है, दो तीन हज़ार कॉपी होते ही किताब बेस्ट सेलर में आने लगती है । डेढ़ सौ करोड़ भारतीयों में कम से कम साठ करोड़ हिन्दी समझते होंगे उसमें से आधे भी शिक्षित हैं तो दो हज़ार प्रतियों के बेस्ट सेलर बन जाने का क्या मतलब हो सकता है?
हिन्दी को असल में संस्कृत की बीमारी लगी हुई है। उसे ज़मीन पर नहीं उतरना है, आकाश में देवलोक में ही लटके रहना है। जैसे संस्कृत गऱीबों से अछूतों से दूरी बनाकर रखती थी, वैसी ही हिन्दी भी है। हिन्दी में सरल और लोक के शब्दों को अपनाने से परहेज़ किया गया है। इसीलिए उर्दू आजकल उपेक्षित होने के बावजूद बहुत समावेशी और हिन्दी से कहीं ज़्यादा समृद्ध बन गई है। उर्दू ने जितने स्रोतों से शब्दों को लिया है वो गज़़ब की बात है। आम आदमी की हिन्दी भी बहुत समृद्ध है लेकिन उस हिन्दी में साहित्य कम ही मिलेगा।
इस कारण बोलने वाली हिन्दी और लिखी/पढ़ी जाने वाली हिन्दी में भारी अंतर पैदा हो गया है। ये अंतर इतना ज़्यादा है कि क्या बतायें।
मैं अक्सर इसे चेक करने के लिए विश्वविद्यालयों के बच्चों से बात करता हूँ। जान बूझकर कोई किताबी हिन्दी शब्द उछाल देता हूँ और सीधे उनकी आँख में झांकता हूँ। वे एकदम नकार देते हैं इन शब्दों को। जैसे ‘वास्तविकता’ ‘समावेश’ ‘आकर्षण’ ‘उपयोग’ ‘विश्राम’ ‘कर्तव्य’ ‘आभास’ ‘अभिव्यक्ति’ ‘आत्मविश्वास’ इत्यादि इत्यादि। वे इन शब्दों के इंगलिश अर्थ पूछते हैं। अगर डेढ़, ढाई, सवाया, पौना, पैंसठ, अठहत्तर, पच्चासी, पचपन जैसे शब्द कह दो तो वे हंसने लगते हैं कि कहाँ के गँवारों वाले शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब इस पीढ़ी से इंग्लिश में भी बात करके देख लीजिए। वहाँ भी वही हाल है। इंगलिश एक तो हमारी भाषा नहीं ऊपर से बिलकुल ही कम पढ़े लिखे प्राइवेट स्कूल के प्राइमरी सेकेण्डरी शिक्षकों से पढ़ी हुई ये पीढ़ी कितनी इंगलिश जान सकती है भला?
छोटे क़स्बे ही नहीं बल्कि अच्छे ख़ासे शहरों के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के शिक्षकों से बात करके देखियेगा। उनके पास कुछ चुनिंदा शब्द होते हैं ‘कीप साइलेंस’ ‘डोंट टॉक’ ‘ओपन योर बुक’ ‘कम हियर’ ‘लिसन केयरफ़ुली’ ‘व्हाट आर यू डूइंग’ ‘व्हाई आर यू लाफि़ंग’ इस तरह के कुछ सिद्ध मंत्र होते हैं जिनके सहारे पहली से बारहवीं कक्षा तक की नैया पार लगती है। क्लास में पढऩे पढ़ाने की बात आते ही वे सीधे किताबें खोलकर ख़ुद पढऩे लगते हैं या दूसरों को रटाने लगते हैं। इंगलिश या हिन्दी में अपने विचार कैसे व्यक्त किए जायें? इस बात से उनका कोई वास्ता ही नहीं होता।
हिन्दी भाषी शिक्षक और छात्र आपस में आसानी से हिन्दी में या हिंग्लिश में बातें करना जानते हैं। लेकिन किताबों पर या सिलेबस के विषय पर किसी भी भाषा में लंबी बात ही नहीं हो पाती। किसी विषय पर टिक कर दस मिनट बात करने का अभ्यास नहीं कराया जाता। कक्षाओ के अंदर छात्रों और शिक्षकों में बड़ा गैप है।
स्कूल तो छोडि़ए यूनिवर्सिटी स्तर तक कक्षाओं में अपने विचार व्यक्त करने की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। अपने-अपने विषय और सिलेबस को रटवाने में ही पूरा समय खर्च होता है। कई बच्चे सिलेबस के बाहर जाकर मुद्दों पर बातें करना चाहते हैं लेकिन अधिकांश शिक्षकों की इस विषय में न रुचि होती है ना ही तैयारी। वे ऐसे छात्रों को हतोत्साहित कर देते हैं, किताब और सिलेबस में उन्हें वापस घसीटकर ख़त्म कर देते हैं।
अनेकों संप्रदायों और दार्शनिक प्रणालियों को जन्म देने वाले भारत के लिए ये एक विचित्र दुर्भाग्य है। हमारा अतीत वाद-विवाद और संवाद से समृद्ध रहा है। लेकिन आज का समय विचित्र है। स्कूल कॉलेज से बाहर सडक़ों पर निकलते ही आपको असली भारत के दर्शन होने लगेंगे। वे बच्चे जो तथाकथित ‘सभ्य और शास्त्रीय’ भाषा के दबाव में क्लास में मुँह नहीं खोलते, वे कॉलेज की कैंटीन में, उनके खेल के मैदानों में, बाज़ार में या किसी मॉल या रेलवे स्टेशन पर आपस में बतियाते हुए, गालियाँ देते हुए मिलते हैं तब उनकी भाषा की कुशलता देखिए, लगता ही नहीं कि ये वही बच्चे हैं जो क्लास में कम बोलते हैं। इसके पीछे बात क्या है?
ये विषय आपस में जुड़ते हैं। ना तो किताबों में न ही कक्षाओं में आम आदमी की भाषा और आम आदमी के मुद्दे छुए जाते हैं। इसीलिए अपनी बोली, भाषा और अभिव्यक्ति में आत्मविश्वास और रुचि पैदा नहीं होती।
संस्कृत की बीमारी से हिन्दी का छुटकारा नहीं हो रहा है। इस कारण हिन्दी अकादमिक भाषा के तौर पर और संपर्क की भाषा के तौर पर भी उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रही है।
कल्पना कीजिए कि साठ-पैंसठ करोड़ की हिन्दी भाषी आबादी के पास ‘क्वांटा’ ‘क्वांटम’ ‘इलेक्ट्रॉन’ ‘स्पेक्ट्रम’ ‘इंटैंगलमेंट’ ‘सिनर्जी’ 'सिंक्रोनिसिटी' इत्यादि जैसे शब्दों का सही अनुवाद और अनुमान ना हो तो क्या होगा? अनुवाद होना ज़रूरी भी नहीं है, इन शब्दों को परिभाषित करके सीधे ही हिन्दी में लिया जा सकता है। इंगलिश ने भी ‘मंत्रा’ ‘योगा’ ‘अवतारा’ ‘पंडित’ ‘गुरु’ जैसे बहुतेरे शब्द परिभाषित करके सीधी सीधे अपना लिए हैं। अभी हाल ही में हिन्दी गलियों का सामान्य शब्द '&तिया' भी इंगलिश में अपना लिया गया है। लेकिन हिन्दी को अभी भी ट्रेन को ‘सहस्रपादविसर्पिणी’ या ‘लौहपथगामीनी’ बनाने की धुन सवार है।
हिन्दी दिवस पर हिन्दी के बारे में हिन्दी में बात करते हुए अक्सर निराशा होती है। अगली पीढ़ी न हिन्दी पढऩा चाहती है ना लिखना चाहती है। वहाँ श्रेणियाँ और जातियाँ बन गई है। हिन्दी में लिखने पढऩे वाले छोटी जाति के हैं, इंगलिश में बोलने लिखने वाले ऊँची जाति के हैं, और इनके बीच छूआछूत की बीमारी फैली है।




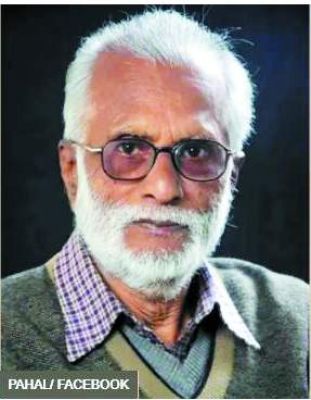

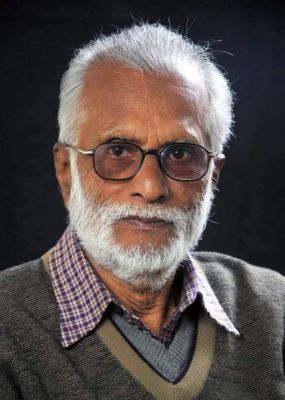


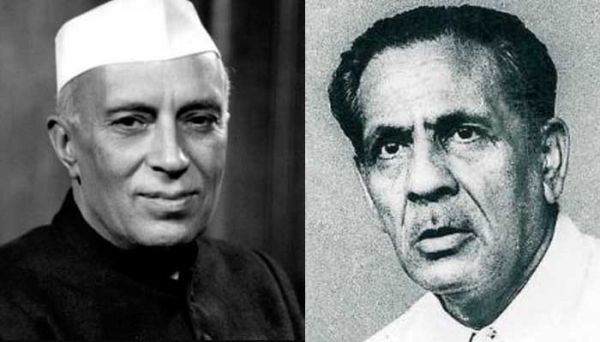
.jpg)
