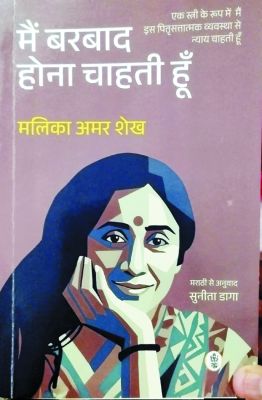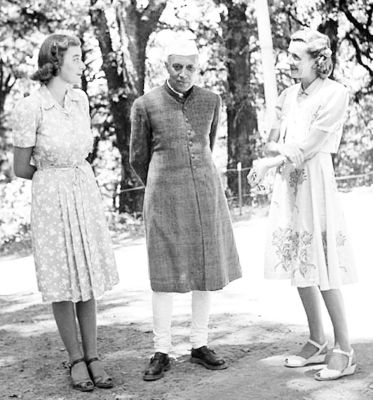विचार / लेख
-अभिनय गोयल
मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 अगस्त) को फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने 16 साल की मुस्लिम लडक़ी की शादी को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत सही ठहराया है।
यह फैसला जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस महादेवन की खंडपीठ ने सुनाया। खंडपीठ ने शादी पर सवाल उठाने वाले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को फटकार भी लगाई है।
आयोग ने लडक़ी की उम्र का हवाला देते हुए शादी पर सवाल उठाया था और इसे पॉस्को अधिनियम (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) का उल्लंघन बताया था।
इस फैसले के बाद बाल विवाह कानून बनाम पर्सनल लॉ की बहस और तेज़ हो गई है। भारत में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत लडक़ी की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है।
समय-समय पर अदालतों, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई अहम फैसले दिए हैं, जिनका मुस्लिम महिलाओं के जीवन पर सीधा असर पड़ा है।
1. जावेद और आशियाना केस
साल 2022 में 26 साल के जावेद और 16 साल की मुस्लिम लडक़ी आशियाना के प्रेम विवाह को हाई कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध माना था।
यह मामला पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में तब पहुंचा था जब दोनों ने अपनी सुरक्षा की मांग की थी। हाई कोर्ट ने शादी को वैध मानते हुए सुरक्षा भी प्रदान की थी।
लाइव लॉ के मुताबिक हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा था, ‘मुस्लिम लडक़ी का विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ से शासित होता है। सर दिनशॉ फरदुनजी मुल्ला की लिखी 'मोहम्मडन लॉ के सिद्धांत' किताब के अनुच्छेद 195 के अनुसार याचिकाकर्ता नंबर 2, सोलह साल से अधिक होने के कारण अपने पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह अनुबंध करने के लिए सक्षम है।’
दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे जफ़रुल इस्लाम ख़ान का कहना है, ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी के लिए लडक़ी की कोई उम्र तय नहीं है। लड़कियों में जब प्यूबर्टी आती है, तब उसे शादी के लायक माना जाता है।’
कोर्ट का कहना था कि इससे बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) का उल्लंघन नहीं होता।
एनसीपीसीआर ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज़ कर दिया।
लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘एनसीपीसीआर के पास ऐसे आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं हैज्अगर दो नाबालिग बच्चों को हाई कोर्ट संरक्षण देता है तो एनसीपीसीआर ऐसे आदेश को कैसे चुनौती दे सकता है।’
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तारीफ करते हुए जफ़रुल इस्लाम कहते हैं, ‘सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मुनासिब है। अंग्रेजों के बाद से ही हिंदुस्तान की हुकूमतों का स्टैंड इस्लामी पर्सनल लॉ में दखल नहीं देने का रहा है।’
वहीं दूसरी तरफ नेशनल काउंसिल ऑफ वूमन लीडर्स की नेशनल कन्वीनर और मानवाधिकार कार्यकर्ता मंजुला प्रदीप का कहना है कि लड़कियों को सामाजिक रीति रिवाज से मुक्त करने की जरूरत है।
बीबीसी से बातचीत में वे कहती हैं, ‘प्यूबर्टी की उम्र में लडक़ी शारीरिक बदलावों से गुजरती है। ये मुश्किल समय होता है। ऐसे में वह खुद शादी जैसे फैसले नहीं ले पाती। उसके फैसले परिवार लेता है।’
‘लड़कियों को मौका मिलना चाहिए कि वे पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हो पाएं और अपने फैसले ले पाएं।’
2. शायरा बानो केस
साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-बिद्दत यानी 'तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
इस मामले की याचिकाकर्ता उत्तराखंड की रहने वालीं शायरा बानो थीं। उनकी शादी साल 2002 में हुई थी। करीब 15 साल बाद उनके पति ने उन्हें एक चि_ी भेजकर तीन तलाक दे दिया था।
पांच जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से फ़ैसला सुनाया था। कोर्ट का कहना था कि यह महिलाओं की समानता और गरिमा के खिलाफ है।
उस वक्त शायरा बानो के वकील बालाजी श्रीनिवासन ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था, ‘ये पहला मौका है जब एक मुस्लिम महिला ने अपने तलाक़ को इस आधार पर चुनौती दी कि इससे उनके मूल अधिकारों का हनन हुआ।’
इस फ़ैसले का कानूनी असर ये हुआ था कि साल 2019 में संसद ने मुस्लिम महिला अधिनियम पास किया। इसके तहत तीन तलाक को गैरकानूनी और दंडनीय अपराध घोषित किया गया।
हालांकि कई धार्मिक संगठनों ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल है।
जफरुल इस्लाम कहते हैं, ‘पर्सनल लॉ को मुस्लिम समाज पर छोड़ देना चाहिए। दीन के जो मसले हैं, उसमें किसी हुकूमत को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए।’
वहीं मंजुला प्रदीप का कहना है, ‘महिला होने के नाते मैं यह कभी स्वीकार नहीं कर सकती कि कोई तीन शब्द बोलकर किसी महिला को खुद से अलग कर दे। ये अन्याय है।’
वे कहती हैं, ‘तीन तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद महिलाओं में हिम्मत बढ़ी है। वे क़ानून का सहारा ले सकती हैं।’
3. हाजी अली दरगाह केस
यह केस मुंबई की मशहूर दरगाह में महिलाओं की एंट्री और बराबरी के अधिकार से जुड़ा है।
2011 के बाद महिलाओं को दरगाह के अंदरूनी हिस्से में जाने से रोक दिया गया था। दरगाह का इंतजाम देखने वाली ट्रस्ट का कहना था कि महिलाओं का दरगाह के अंदर जाना धार्मिक नियमों के ख़िलाफ़ है।
इसके खिलाफ भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। साल 2016 में कोर्ट ने महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया।
कोर्ट का कहना था कि ट्रस्ट धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देकर महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना था।
यह फैसला महिलाओं की धार्मिक स्थलों में बराबरी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। इसके बाद सबरीमाला मंदिर और शनि शिंगणापुर मंदिर जैसे मामलों में महिलाओं के जाने को लेकर कानूनी बहस तेज हुई।
4. शाह बानो केस
यह मामला मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई में मील का पत्थर माना जाता है।
इंदौर की रहने वाली शाह बानो का साल 1932 में निकाह हुआ था। उनके पांच बच्चे थे।
साल 1978 में 62 साल की शाह बानो ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपने पति मोहम्मद अमहद ख़ान से तलाक के बाद हर महीने 500 रुपए गुजारा भत्ता की मांग की।
उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता(सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ते की मांग की थी। उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने तर्क दिया था कि भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तलाक के बाद पति इद्दत की मुद्दत तक ही गुजारा भत्ता देता है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक इद्दत वह अवधि होती है, जब एक पत्नी अपने पति की मौत या तलाक के बाद बिताती है। ये तीन महीने का समय होता है, लेकिन स्थिति के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है। इस मामले पर लंबी सुनवाई चली। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट का कहना था कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी नागरिकों पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो।
फैसले को मुस्लिम महिलाओं के लिए जीत माना गया है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग ने इसका विरोध किया और इसे शरीयत में दखल करार दिया। विरोध के दबाव में एक साल बाद राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक पर संरक्षण अधिनियम), 1986 पास कर दिया। इसकी नतीजा ये हुआ कि शाह बानो के मामले पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट गया और कहा गया कि इद्दत की अवधि के लिए ही भत्ता दिया जा सकता है।
5. डेनियल लतीफ़ी केस
यह मामला शाह बानो केस से सीधा जुड़ा हुआ है। शाह बानो केस में वकील डेनियल लतीफी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की।
इस याचिका में उन्होंने राजीव गांधी सरकार के मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) कानून, 1986 की वैधता को चुनौती दी थी।
कोर्ट ने अधिनियम की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा था, ‘मुस्लिम पति का अपनी तलाकशुदा पत्नी के प्रति भरण-पोषण का दायित्व इद्दत अवधि तक सीमित नहीं है।’
फैसले में कहा गया था कि पति को इद्दत की अवधि में ही जीवनभर के लिए गुजारा भत्ते की व्यवस्था करना होगी।
इस फैसले ने मुस्लिम महिलाओं को लंबी अवधि के लिए आर्थिक सुरक्षा दिलाई। (bbc.com/hindi)