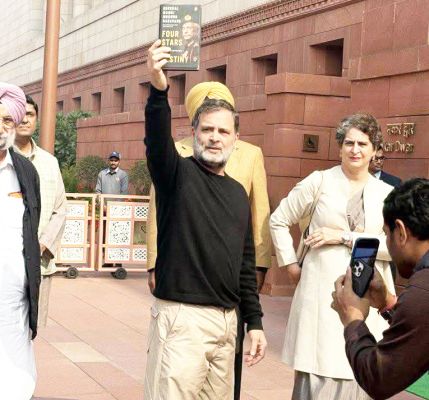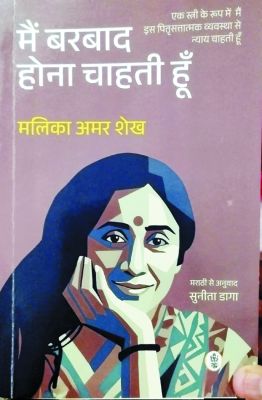विचार / लेख

-दिनेश चौधरी
नगर पालिका कार्यालय के प्रवेश-द्वार के ठीक सामने चारदीवारी से घिरा एक बड़ा-सा कमरा था। इसी कमरे में सार्वजनिक वाचनालय हुआ करता था। अपना घर नगर-पालिका के पीछे थे। पीछे लोहे की सलाखों वाला गेट था और दो सलाखों के बीच इतना अंतराल था कि अपने सिर को धँसा दिया जाए तो वह आसानी से प्रवेश कर जाता था। एक बार सिर अंदर चला गया तो कंधों को समकोण पर मोड़ लेने से पूरी देह आर-पार हो जाती है। अंदर ठीक सामने जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्यालय था और इसके बाद मुख्य कार्यालय। यह लाइब्रेरी जाने का अपना ‘शार्टकट’ था। यानी घर से लाइब्रेरी जाने में बमुश्किल डेढ़-दो मिनट लगते रहे होंगे। लाइब्रेरी के पीछे एक छोटा-सा मैदान था, जो हमारे खेलने के काम आता था।
वाचनालय का मासिक शुल्क दो रुपये था। लकड़ी और काँच से बनी किताबों की आलमारियां दीवार से लगी होती थीं। लाइब्रेरी में प्रवेश करते ही दायीं ओर लाइब्रेरियन की मेज और कुर्सी थी और इसके ठीक ऊपर गांधीजी की मढ़ी हुई लोकप्रिय फोटो, जिस पर स्थायी रूप से प्लास्टिक की माला चढ़ी होती। स्थायी ग्राहक होने के कारण लाइब्रेरियन से अपनी पक्की दोस्ती थी। लाइब्रेरी खुलने से पहले ही आस-पास भीड़ जमा हो जाया करती थी और जैसे ही दरवाजा खुलता लोग झुंड में टूट पड़ते। इस आतुरता की वजह नई पत्रिकाओं को हथियाने की होती थी। पत्रिकाओं में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, माया, मनोहर कहानियां, सत्य कथा, सरिता, मुक्ता, कादम्बिनी, सारिका, माधुरी और मायापुरी वगैरह हुआ करती थीं। बच्चों की पत्रिकाओं में पराग, नन्दन, चंदामामा और बाल भारती होती थीं।
कॉमिक्स इस लाइब्रेरी में नहीं आती थी। तब ‘लोटपोट’ और ‘मधु मुस्कान’ बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। अपने क्लास में कुछ सिंधी सेठों के बच्चे हुआ करते थे जो पढऩे में फिसड्डी थे। इनके यहाँ कॉमिक्स का ढेर लगा होता था, पर ये किसी को देते नहीं थे। इनके साथ अपना एक समझौता था। अपन होमवर्क में इनकी मदद करते और वे बदले में पढऩे के लिए कॉमिक्स देते। एक ‘दीवाना’ नाम की पत्रिका भी मुझे याद आ रही है। फैंटम और जादूगर मेंड्रेक की सीरीज रोज अखबारों में आती थी। जादूगर मेंड्रेक की लोथार के साथ जोड़ी वैसे ही पॉपुलर थी, जैसे चाचा चौधरी की साबू के साथ। फैंटम का ट्री हाऊस हाऊस हुआ करता था और उसके परिवार में पत्नी डायना और जुड़वाँ बच्चे रैक्स और लुई भी हुआ करते थे। कोई नाम-वाम गलत आ जाए, तो कृपया ठीक कर लें।
नई पत्रिकाएँ घर ले जाने नहीं मिलती थीं, उन्हें लाइब्रेरी में ही पढऩा होता था। साहित्यिक किताबों को लेकर कोई बंदिश नहीं थी। चूंकि इसके ग्राहक कम थे, इसलिए कितनी भी मात्रा में किताबे रजिस्टर में दर्ज कर घर ले जाई जा सकती थीं। लाइब्रेरियन आलसी था। किताबों और लेखक के नाम दर्ज करने के बदले सिर्फ संख्या दर्ज करता था। इसका भरपूर लाभ अपने एक परिचित ने उठाया, जिनके घर में वाचनालय की आधी से अधिक किताबे पायी जाती थीं। उन्हें कोई अपराध-बोध भी नहीं था, उल्टे वे इस बात का उल्लेख बड़े गर्व के साथ करते थे। उनसे प्रभावित होकर यशपाल की ‘चक्कर क्लब’ और ‘बात बात में बात’ मैंने भी उड़ाने की ठान ली थी, फिर सोचा कि अच्छी किताब है तो औरों के भी काम आनी चाहिए। दोनों बड़ी मजेदार किताबें थी। इसमें कामरेड किस्म के जीव मुफ्त की चाय-पकौड़ी के जुगाड़ में रहते हैं और मध्यमवर्गीय परिवारों में बतरस का आनन्द लेते हुए अपनी बात कह जाते हैं। निराला से लेकर बच्चन तक की किताबें यहाँ उपलब्ध थीं। ‘अंधा संगीतज्ञ’ भी यहीं मिलती थी और चेखव की कहानियां भी। विदेशी साहित्य मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाता क्योंकि पात्रों और शहरों के नाम मुझे याद नहीं रहते। मुझे लगता कि अनुवादक जब अनुवाद में इतनी मेहनत करते हैं तो उन्हें पात्रों को भी मोहन-सोहन और गाँव-शहरों को रामपुर-श्यामपुर कर देना चाहिए, ताकि पढऩे में जरा आसानी हो जाए। ब्लादिमीर नोबोकोव जैसे नाम पढऩे में ही पसीना छूटता था। फिर भी जो थोड़ा-बहुत पढ़ पाया, उसका संस्कार यहीं से मिला।
लाइब्रेरी में बहुत तरह के लोग आते थे। ज्यादातर रिटायर्ड या अधेड़ उम्र के। नन्दन-पराग के चक्कर बच्चे भी खूब होते थे, अलबत्ता युवा कम ही दिखते थे। फिर भी आज के माहौल को देखते हुए उस संख्या को ठीक-ठाक कहा जा सकता है। आजकल के छोकरों की दिलचस्पी जिम जाने में ज्यादा है। जिम जाकर छ: या आठ एप बनाने से सेल्फ़ी अच्छी आती है, जबकि तब न जिम थे न सेल्फी। तो बेचारी युवा पीढ़ी को मजबूरी में लाइब्रेरी ही जाना पड़ता था और ‘आजाद लोक-अंगड़ाई’के चक्कर में वे सार्वजनिक क्षेत्र के बजाय निजी क्षेत्र की लाइब्रेरी को चुनना पसन्द करते थे। निजी क्षेत्र की लाइब्रेरी दो किस्म की होती थी; एक स्थायी जो साल भर चलती थी और दूसरी अस्थायी जो केवल गर्मियों की छुट्टियों में खुलती थीं। छोटे से छोटे कस्बे में इस तरह की 8-10 लाइब्रेरियाँ तो होती ही थीं। तब एक सिटिंग में नॉवेल पढऩा गर्व का सबब होता था और मोहल्ले में यह बात बाकायदा ऐलान के रूप में बताई जाती थी। किशोर उम्र के बालकों के लिए निजी लाइब्रेरी में राजन-इकबाल सीरिज वाली एस.सी. बेदी की किताबें हुआ करती थीं।
निजी क्षेत्र की लाइब्रेरी में भिलाई की ‘अपना पुस्तकालय’ से अपना विशेष नाता रहा। इसकी दो शाखाएँ थीं, एक सेक्टर -6 में और दूसरी सेक्टर-10 में। कोई और भी रही हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। यहाँ भीड़ ऐसी उमड़ती थी, मानों शहर भर के लोगों ने इसकी सदस्यता ले रखी हो। सुबह-शाम इसके खुलने से पहले ही लोगों की भीड़ जमा होनी शुरु हो जाती थी। लाइन भी लगती थी। किताबों को लेकर कोई बंदिश नहीं थी। 8-10 किताबें, जितनी भी चाहें निकलवाई जा सकती थीं, बशर्ते पुरानी जमा कर दी गई हों। अब तक जो कुछ भी पढ़ा, उसका एक बड़ा हिस्सा यहीं से मिला। पहली बार ‘राग दरबारी’ भी यहीं से लेकर पढ़ी। एक सज्जन हमेशा कविताओं की किताब ले जाते थे। मैंने उनसे पूछा ‘‘आप नॉवेल नहीं पढ़ते?’’ उन्होंने कहा कि ‘‘वो तो खरीद लेता हूँ।’’ मैने पूछा, ‘‘फिर कविताएँ क्यों नहीं लेते?’’ उन्होंने हँसते हुए कहा, ‘‘ये किताबें मुझे जरा महंगी लगती हैं। एक तो पहले ही शब्द-संख्या बहुत कम होती है। फिर दो-चार समझ में नहीं आईं तो और नुकसान!’’ तभी यह मौलिक ख्याल मेरे जेहन में आया कि अगर शब्दों को तोलकर बेचा जाता तो भारी मात्रा में लेखन करने वाले प्रेमचन्द जैसे लेखक फ़टे जूते पहनकर नहीं घूमते।
इसी दौर में सुरेंद्र मोहन पाठक की किताबें पढऩे का चस्का भी लगा। बड़े भाई साहब ने बताया था कि इनके नॉवेल ठीक-ठाक होते हैं। दो-तीन किताबें पढ़ीं। मजा तो आने लगा पर ‘पथभ्रष्ट’ होने का अपराध-बोध भी। एक सिटिंग में नॉवेल खत्म करना क्या होता है, यह समझ में आने लगा था। दूसरी ओर से आत्मा धिक्कार रही थी। साहित्यानुरागी का ऐसा विचलन! साँप-छछूँदर वाली स्थिति हो रही थी। तभी श्रीलाल शुक्ल की दो किताबें मिलीं, ‘मकान’ और ‘आदमी का जहर।’ ‘मकान’ बेशक ‘राग-दरबारी’ नहीं थी पर इसका शिल्प भी कुछ अलग हटकर ही था और मुझे आज भी लगता है कि इसकी चर्चा जरा कम ही हो पाई। ‘आदमी का जहर’ पढा तो सकते में आ गया। दोबारा लेखक का नाम देखा। फिर किसी से पुष्टि की कि ‘हाँ, ये वही श्रीलाल शुक्ल हैं।’ किसी और ने बताया या शायद कहीं पढा कि मुक्तिबोध भी जासूसी नॉवेल पढ़ते थे। इन सबका मिला-जुला असर ये हुआ कि मन में बैठा हुआ अपराध- बोध चल बसा और सुरेंद्र मोहन पाठक के साथ जेम्स हैडली चेज के सारे उपलब्ध नॉवेल पढ़ डाले। आगे तो यह भी होता रहा कि पाठक की कोई नॉवेल खरीद कर लेते, उसे जरा सावधानी के साथ पढ़ते कि कहीं पन्ने वगैरह न मुडें और फिर उसी दुकान से उस किताब के बदले में कोई दूसरी किताब चौथाई मूल्य पर ले लेते। नई किताब के आने का इंतज़ार भी बड़ी बेसब्री के साथ किया जाता। विमल सीरीज की किताबों का तो जैसे मुझे नशा ही हो गया था।
इससे पहले इब्ने शफी, कर्नल रंजीत और ओमप्रकाश शर्मा पर भी अपन हाथ आजमा चुके थे। ओमप्रकाश शर्मा को तब ‘जनप्रिय लेखक ओम प्रकाश शर्मा’ कहा जाता था और जगत, जगन, गोपाली वगैरह उनके लोकप्रिय पात्र हुआ करते थे। तब बहुत से घरों में इन उपन्यासकारों का प्रवेश वर्जित हुआ करता था। जिन्हें मध्यमवर्गीय परिवारों में मान्यता थी, वे ‘सामाजिक’ उपन्यास कहलाते थे और इनमें गुलशन नंदा का नाम अव्वल था। रानू और राजवंश भी हुआ करते थे। कोई एक कुशवाहा कांत भी थे, जो क्या लिखते थे अब याद नहीं आ रहा। वेद प्रकाश शर्मा का भी एकाध नॉवेल पढऩे की मैंने बहुत कोशिश की, पर नहीं पढ़ सका। इन लेखकों को भले ही साहित्य में कोई जगह न मिल पाई हो पर इतना तो उदारतापूर्वक स्वीकार किया ही जाना ही चाहिए कि इन्होंने एक बड़े तबके के बीच पढऩे की आदत को विकसित किया, जो अब नितांत दुर्लभ हो चली है।
नगर पालिका वाली लाइब्रेरी में आने वाले रिटायर्ड लोगों में एक यदु अंकल हुआ करते थे। वे दिल्ली प्रेस की ‘सरिता’ के घनघोर प्रशंसक थे और उसका इतना प्रचार करते थे, जितना अमिताभ बच्चन ने नवरतन तेल का भी नहीं किया होगा। ‘सरिता आई क्या’ उनका तकिया कलाम बन गया था और वे यह सवाल हर तीसरे दिन पूछते थे, जबकि पत्रिका पाक्षिक थी। पत्रिका का नया अंक आया हो और सबसे पहले उन्हें हासिल न हो तो वे हंगामा काट देते थे। एक दिन एक अलग समूह में कुछ अधेड़ पाठक आपस में बातें कर रहे थे और उनमें से किसी ने कहा कि ‘सरिता आ गई है।’ यदु अंकल के कान खड़े हो गए। वे लपक कर वहाँ पहुँचे और जान न पहचान उनसे पूछने लगे कि ‘सरिता कहाँ है?’ वे सज्जन बेचारे थोड़े संकट में पड़ गए। फिर भी जवाब दिया कि घर में है। यदु अंकल आनन-फानन में लाइब्रेरियन के पास पहुँच गए और लडऩे लगे कि जब पत्रिका इश्यू नहीं की जाती है तो घर कैसे पहुँच गई। बाद में पता चला कि जिन सज्जन ने ‘सरिता आ गई है’ वाली बात कही थी, वह सच्ची थी पर सरिता उनकी पत्नी का नाम था जो अपने मैके गई हुई थीं। इस घटना के बाद बेचारे यदु अंकल 6-7 दिन तक लाइब्रेरी नहीं आए। मैं लाइब्रेरियन से धीरे से पूछता ‘सरिता आई क्या’ और फिर हम दोनों धीरे से मुस्कुरा उठते।
फिर 1982 में एशियाई खेलों के बहाने टीवी का प्रसार हुआ। ‘फिश बोन’ आकार वाले एंटीना कुकुरमुत्तों की तरह छतों में उग आए। एक टीवी इसी लायब्रेरी में भी आया। खेलों का मामला था। टीवी दिन भर चलने लगा। फिर चित्रहार और सिनेमा वगैरह आने लगे, सीरियल चालू हुए। टीवी धीरे-धीरे सस्ते होने लगे और न्यूज प्रिंट व कागज वगैरह के दाम बढऩे लगे। टीवी जितना फैलता जा रहा था, पत्रिकाएँ उतनी सिमटती जा रही थीं। एशियाई खेलों के दौरान टीवी केंद्र का उद्घाटन करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि टीवी के आने से वैज्ञानिक चेतना का प्रसार होगा। क्या हुआ यह सबने देखा। टेक्नोलॉजी पर बाबाओं ने कब्जा कर लिया। भूत-प्रेत के सीरियल आने लगे। अंधविश्वास को विज्ञान साबित किया जाने लगा। मिथकीय गुफाओं-कन्दराओं-पहाडिय़ों की खोज की जाने लगी और एक दिन हम सबने देखा कि अचानक मूर्तियां दूध पीने लगीं। इस बीच धर्मयुग, सारिका, साप्ताहिक हिंन्दुस्तान, दिनमान, रविवार वगैरह बन्द हो चुके थे। फिश बोन एंटीना ने हमारे घरों में दीमक की फौज घुसा दी थी। कवि कहता है, ‘दीमक किताबें नहीं पढ़तीं, दीमक किताबें चाट जाती हैं।’