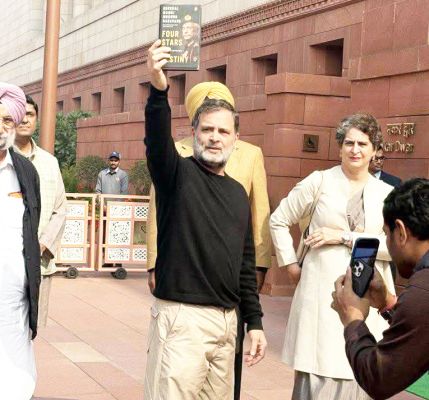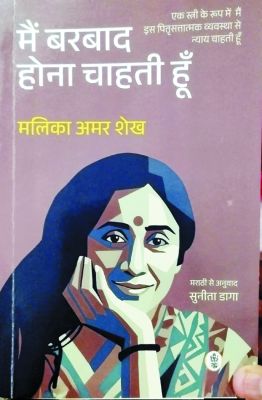विचार / लेख

2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों (अनुसूचित जनजातियों) की जनसंख्या 10,42,81, 034 है। वह देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। बोलियों, भाषाओं, जनसंख्या तथा रहन-सहन आदि को लेकर आदिवासियों में कई विविधताएं हैं। पूर्वोत्तर राज्य समूह मोटे तौर पर तिब्बती, बर्मन, माॅन-खमेर तथा भारतीय-यूरोपीय जैसे तीन मुख्य समूहों में वर्गीकृत किये जाते हैं। कुछ जनजातियां बहुत पिछड़ेपन के कारण अतिसंवेदनशील जनजातीय समूहों में रखी गई हैं।
आदिवासियों ने राष्ट्रीय जीवन में ज्यादातर एकांत में रहते सुदूर तथा बीहड़ जंगली क्षेत्रों में लगभग आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत किया है। प्रशासनिक तंत्र उनको अलग थलग रखने और राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा से नहीं जोड़ने की रुचि में रहता आया है। स्वतंत्रता के बाद संविधान ने जनजातीय लोगों को विशेष दर्जा देने के लिए कई प्रावधान बनाए। संसद ने कई सुरक्षात्मक कानून बनाकर उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए सजग प्रयास किये। सभी कोशिशों के बावजूद सच यही है कि आदिवासियों के जीवन स्तर में केवल मामूली सुधार आ पाया है। अनुसूचित जनजाति का मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) बाकी जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। साक्षरता दर में भी अंतर बहुत है। गरीबी रेखा के नीचे अन्य समुदायों की अपेक्षा अनुसूचित जनजातीय परिवार ज्यादा हैं। आरक्षण के प्रावधान के बावजूद सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिशत उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं ही है। इस तरह उनकी हालत बाकी लोगों की अपेक्षा काफी खराब है।
आदिवासियों के लिए बनाए गए (1) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA), (2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, (3) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009, (4) भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनरव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2003, (5) पंचायत के प्रावधान अनुसूची क्षेत्रों में विस्तारण अधिनियम, 1996 (PESA), तथा (6) संविधान की पांचवीं एवं छठी अनुसूची के प्रावधान कठोरतापूर्वक लागू नहीं किये जाते। उसके चलते उनके विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।
जनजातियों में साक्षरता की कमी है। आदिवासी अपने कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी नहीं रखते। कई जनजातीय लोग कथित रूप से नक्सली कहकर जेलों में डाले जाते हैं। न्यायिक कार्यवाहियां तो जनजातियों को अदालतों में डराती ही हैं। वे प्रशासनिक अराजकता से भी पीड़ित होते हैं। कई अनुसूचित जनजातियां वनवासी हैं। उनके निवास क्षेत्र आरक्षित वन तथा सुरक्षित वन घोषित कर दिए गये हैं। उन्हें बिना मुआवजा हटा दिया जाकर बेदखल कर दिया जाता है। सभी जनजातियां अनुसूचित जनजातियों का दर्जा भी नहीं प्राप्त कर सकी हैं। इसके चलते इन जनजातियों की हालत खराब है। उन्हें पांचवीं अनुसूची एवं पेसा के प्रावधानों द्वारा दिए गये अधिकार एवं सुरक्षा नहीं मिलते। इन वर्गों के लिए वन अधिकार अधिनियम ढीले ढाले तौर पर लागू किया है।
जंगल तथा पहाड़ियां जनजातीय पहचान के मुख्य स्त्रोत हैं। भूमियों का एक बड़ा भाग वन क्षेत्रों में आता है। दूरदराज क्षेत्र की अधिकतर जनजातियां उन जमीनों में बिना किसी अधिकार, हक हुकूक एवं हित के वन भूमि पर रहती आई हैं। उन बेघर जनजातियों हेतु वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उनके अधिकारों की सुरक्षा एवं बसाहट हेतु कोई स्पष्ट और अमलकारी विधिक प्रावधान नहीं हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनरुद्धार एवं पुनर्वास में उचित मुआवजे एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत जनजातियों को दिया गया मुआवजा अक्सर कम होता है। जनजातियों के साथ एक अन्य समस्या और है। भूमि पर एकल अधिकार की जगह वे सामुदायिक अधिकार में विश्वास रखते हैं। इसलिए भूमि संबंधित मामलों में उनके पास स्वामित्व का लिखित प्रमाण नहीं होता। जनजातियों के दावे अधिकतर मौखिक साक्ष्य पर ही आधारित होते हैं। नतीजतन उनके मालिकी हक स्थापित करने में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। जनजातियों को प्रमाणीकरण एवं दावों के निपटारे के पहले ही बेदखल कर दिया जाता है। इसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति और पारंपरिक वन प्रथाओं में गिरावट आ रही है।
शिक्षा, टरेनिंग, नगरी सभ्यता से वंचित तथा औपचारिक संचार संसाधनों वगैरह की कमी के बावजूद आदिवासी वन के एडवेंचर पर ही निर्भर रहा है। आदिवासियों ने सदियों में दुर्लभ खेती करने की अपनी पद्धति का आविष्कार भी कर लिया। खेती भी उनके आर्थिक जीवन का एक बुनियादी साधन है। कृषि की कई नई देशज तक्नालाॅजी और प्रविधियों को भी उन्होंने एक तरह से स्वयमेव ईजाद किया। उनकी दैहिक तथा दैनिक जरूरतें न्यूनतम होती हैं। उन्हें आजकल के लोकप्रिय अंगरेजी शब्द ‘मिनिमल‘ (अल्पतम) के अर्थ में औद्योगिक पश्चिमी सभ्यता के दंश से पीड़ित लोग भी आदत में शुमार कर रहे हैं।
सुंदर और दुरूह पहाड़ियों तथा जंगलों के माहौल में आदिवासी न जाने हजारों वर्षों से जीवित और स्वायत्त रहते आए हैं। प्रकृति के कई आकस्मिक प्रकोप मसलन भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, सूखा, अतिवृष्टि वगैरह भी उन्हें विचलित नहीं कर पाए। प्रकृति को जीतने का उनमें न तो कोई नवसाम्राज्यवादीनुमा अहंकार रहा और न ही उन्होंने उस प्रकोप को खुद की किसी पापजनित गतिविधि का दंड समझा। राज्य की किसी भी केन्द्रीय शक्ति या संस्था से उनका सरोकार बेरुख होने के कारण नहीं रहा है। राज्यशक्ति ने भी उनसे भौतिक, सामाजिक और आधिकारिक दूरी बनाए रखी। हालांकि उन्हें उपेक्षित करने का विचार शुरुआती राज्यतंत्र का अनिवार्य अंग भी नहीं बना।
भारतीय आदिवासी जीवन में सबसे पहला, बड़ा, परिणामकारी और घुमावदार मोड़ ब्रिटिश हुकूमत के भारत में पैर जमाने के बाद आया। आदिवासियों ने कथित नागरिक सभ्यता के धारकों से कहीं पहले वीरोचित अर्थ में बर्तानवी अत्याचार का खुलकर मैदानी मुकाबला भी किया। ब्रिटिश शासन ने ‘अपवर्जित क्षेत्र‘ और ‘आंशिक अपवर्जित क्षेत्र‘ का वर्गीकरण आदिवासी इलाकों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्तदुरुस्त करने की आड़ में किया। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ‘अपवर्जित क्षेत्र‘ और शेष भारत के आदिवासी इलाकों के लिए ‘आंशिक अपवर्जित क्षेत्र‘ की शासकीय परिभाषा रची गई। संविधान की छठी अनुसूची इसी बात को ध्यान में रखकर पूर्वोत्तर के सघन आदिवासी इलाकों के संदर्भ में अधिनियमित की गई। उसके तहत आदिवासियों की परंपराओं, रूढ़ियों, संस्कृति, सामाजिक प्रबंधन, आर्थिक तंत्र और वन तथा वनोत्पादों के अधिकारों सहित कृषि के पुराने पैटर्न ने कम से कम मात्रा में छेड़छाड़ करना शामिल किया। शेष भारत के आदिवासी क्षेत्रों के लिए पूर्वोत्तर के मुकाबले नागर सभ्यता से बेहतर संपर्क, आवागमन के साधन, अन्य संचार व्यवस्था, भौगोलिक रचना और ज्ञात अज्ञात कई कारणों से पांचवीं अनुसूची की रचना का कूटनीतिक फैसला ब्रिटिश बुद्धि की प्रेरणा से भारतीय संविधान सभा ने अधिनियमित कर दिया। उसके अनुसार केन्द्र अथवा राज्य शासन तथा राज्यपाल के संवैधानिक उत्तरदायित्व के तहत आदिवासी विकास के नाम पर उनकी कथित यथास्थिति की सदियों पुरानी जीवन पद्धति को ही खंडित कर दिया।
भारत वैसे भी सदियों से ग्रामीण सभ्यता, लोकसंस्कृति, गणतांत्रिक व्यवस्था, प्रकृति-निर्भर जीवन पद्धति और नए जीवन मूल्यों को विकसित करने की प्रजातांत्रिक परंपराओं से जूझते रहने का इतिहास रचता रहा। इतर आदिवासी इलाके के ग्रामीण क्षेत्रों तथा उनके बरक्स आदिवासी इलाकों में परिवर्तन के ढांचे के मूलभूत तत्वों में काफी अंतर देखने में आता रहा है। नागर सभ्यता में वर्ग और वर्ण की व्यवस्था के उद्भव तथा विकास हो जाने के कारण समाज अपने तकनीकी, तात्विक, वास्तविक और संगठनात्मक स्तर पर विभाजित और खंडित होते होते अब तो लगभग खंडित हो ही गया है।
आदिवासी जीवन की आवश्यकताएं शासकीय, शहरी या अन्य तथाकथित सभ्य इलाके में औपचारिक रूप से विकसित बाजारतंत्र के अर्थशास्त्र पर निर्भर नहीं रही हैं। न ही उन्हें उसकी ज़रूरतें महसूस हो पाईं। एक लंबे अरसे तक उनके लिए कुदरत और जंगल तथा अन्य वन स्त्रोत और वन-उत्पाद ही सामाजिक, आर्थिक और वास्तविक जीवन का आधार रहे हैं। उनमें गरीब और अमीर, साधनसंपन्न और साधनविहीन, उच्च वर्ग या अकिंचन जैसे अन्दरूनी भेद विभेद नहीं रहे। इस कारण उनका कोई एक उपवर्ग या हिस्सा गरीबी और भुखमरी की कगार पर खड़ा होने को मजबूर नहीं हुआ। इसके ठीक उलट आधुनिक सभ्यता ने विभाजन, विग्रह और विसंगत दंश झेले हैं। शासक, नगरसेठ, नौकरशाह, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, अछूत और अकिंचन जैसे सैकड़ों शहरी विशेषण हैं। ये कथित विकसित और आधुनिक सभ्यताओं के माथे पर कलंक की तरह चिपकाए जा सकते हैं। जंगल आदिवासी के केवल आर्थिक सहकार का परिवेश नहीं रहा। अपनी प्राकृतिक संरचना के कारण आदिवासी जीवन संगीत, संस्कृति, कलात्मक उद्भव और पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और अनुकूलन जैसी अब तक अबूझ और अनोखी अंतर्लय को विकसित करते रहने का विश्वविद्यालय होता गया है। जंगल से आदिवासी का विलग होना कल्पनातीत बात रही है। उसने कभी भी वन की सरहदों को लक्ष्मणरेखा की तरह स्वीकार नहीं किया। ब्रिटिश हुकूमत व्यवस्था से शुरू होकर आज तक उसी शासन पद्धति का दबदबा कमोबेश कायम है। इस प्रकल्प का भारतीय आदिवासी जीवन पर सीधा और घातक असर अंगरेजों के शासन काल से शुरू होकर स्थायी होता लग रहा है।
आदिवासियों ने सदियों में सिद्ध किया कि जीवन की सामूहिकता, मनुष्यों की अंतनिर्भरता के साथ साथ सामाजिक मूल्यों के उद्भव, विकास और अनुपालन के लिए अकादेमिक शिक्षण, मशीनी शासन तंत्र और जीवन मूल्यों को समझने की दृष्टियों के उन्नयन की आड़ में विग्रहों को अंतस्थ करना कतई आवश्यक नहीं है। आदिवासी को तथाकथित विकास योजनाओं के नाम पर सदियों से निवास कर रहे स्थानों से बेदखल करना, उन्हें आवासहीन बनाकर शहरी परिवेश में लगभग प्रदूषित इलाकों में स्थानांतरित कर मजदूरी वगैरह के अनिच्छुक कामों में जबरिया खपा देना और आदिवासी इलाकों में सिंचाई उद्योग, वन प्रबंधन, विद्युत वगैरह के कई उपादानों का काॅरपोरेटी सरंजाम खड़ा कर आदिवासी क्षेत्रों की सामाजिक संरचना को शहरी संपर्क से जोड़कर क्षतिग्रस्त करना भी तो हुआ।
यूरोपीय जीवन पद्धति, विदेशों में आवागमन तथा शिक्षण और व्यापार के लिए भारतीयों का प्रवास, आर्थिक व्यवस्था में मशीनीकृत ढांचे का उपयोग और उद्भव, शिक्षा के ढांचे में मूलभूत और मशीनी व्यवस्था पर निर्भर तंत्र आधारित विकास, व्यापार के नाम पर बाजारवाद का नया ककहरा ये सब कारक रहे हैं। ऐसे सोच को जब भारतीय शहरी साभ्यतिक जीवन से ही कोई परहेज नहीं था, तो आदिवासियों की निपट निरक्षरता, सादगी, अहिंसकता और मासूमियत के रहते उनका शोषण कर लेना अपेक्षाकृत सरल था।
एक कुटिल विधायन भारतीय वन अधिनियम के नाम से किया गया। आदिवासियों के पुश्तैनी व्याकरण में छूट, कंसेशन, लाइसेंस, परमिट, अनुमति आदि नए शब्दों को ठूंसते उनमें अधिकारविहीनता, लाचारी, निराशा और लुट जाने का मनोवैज्ञानिक भावबोध इंजेक्ट कर दिया गया। प्रशासनिक कुटैव द्वारा लादी गई यह मानसिकता तात्कालिक नहीं, स्थायी चरित्र की हो गई है। आजादी के बाद जनप्रतिनिधियों द्वारा रचित इतिहास के पहले संविधान में भी वह समीकरण हल नहीं किया गया जो पेचीदा प्रबंधन अंगरेज स्वातंत्र्योत्तर भारत के शासकों को सौंप देने के लिए कैबिनेट मिशन योजना के कुटिल चक्र में फंसाकर चले गए थे। कुदरती परंपराओं, स्मृति संचयन, व्यावहारिक बुद्धि और आंतरिक आग्रहों को दाखिलखारिज करते वन विभाग नाम का शासन तंत्र का प्रतिनिधिक रोबोट आदिवासी जीवन की मुश्कें बांधने के लिए जंगलों का एकाधिकारी बना दिया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया। सरकारी बेड़ियां आदिवास को अपनी भृकुटि, तांत्रिकता, शोषण और दोहन की मुद्राओं में लगभग क्रूर होकर जकड़ती चली गईं। नए दौर के युवा आदिवासियों तथा कई ठूंठ बना दी गई पुश्तैनी व्यवस्थाओं ने यह भी अहसास कर लिया है कि शासन उनके पुश्तैनी आत्मानुशासन के मुकाबले शायद श्रेष्ठतर विकल्प है। उसके सामने झुकने और आज्ञाकारी बनते रहने के अलावा अब उनके जीवन में कोई ठौर नहीं है।
शासनतंत्र जानबूझकर ऐतिहासिकता पर क्रूरता का पोचारा फेरता रहा है कि व्यापक भारतीय सामाजिक जीवन का सबसे ज्यादा अनोखा, मानवीय, प्रकृतिसंपन्न, दार्शनिक वृत्तियों का जीवनांश ही यादों के इतिहास से धुंधला होता होता पूरी तौर पर मिटाया जा रहा है। सत्ता नाम का शब्द सभ्यता, संस्कृति, संगीत, सामाजिकता और सामूहिकता पर इस कदर हावी हो गया है जैसे मनुष्य जीवन के सभी स्वाभाविक अवयव अपनी निर्दोषिता, मासूमियत और सकारात्मकता के बावजूद मानो किसी आॅक्टोपस की जकड़ में कैद हो जाएं।
आदिवासी जीवन में हस्तक्षेप करने उसके विस्थापन का भ्रूम इंजेक्ट कर दिया गया। ऐसे तिलिस्म के भविष्य की आदिवासी कल्पना ही नहीं कर सकता था। भूमि का आदिवासी-अर्थ उसके लिए ऐसा क्षेत्र या इलाका है, जहां सहकार और सामूहिकता के जरिए ही संपत्ति का बोध उसके सामाजिक अधिकार का अहसास बनकर उसमें समाता रहा है। सरकारी हुक्मनामे के कारण आदिवासी अपनी पुश्तैनी समझ से ही बेदखल कर दिया गया। उसे समझ नहीं आया कि जिस भूमि पर वह कभी कभार, यूं ही या अमूमन हर सम्भावित स्थिति में भी समाज के अंश के रूप में काश्त करता था, अब भूमि का उतना टुकड़ा ही उसका खुद का अधिकार कहलाएगा। यह तो भूमिस्वामी को ही एक तरह से खुद की भूमि का नया मुख्तारनामा पाना सिद्ध हुआ। उस कथित स्वामित्व का सीधा रिश्ता सरकार नामक अदृश्य लेकिन हर जगह उपस्थित दमनकारी संस्था से हो गया।
मालिक बनी संस्था ने पटवारी नाम का स्थानीय राजस्व अधिकारी बनाया। पटवारी के अधिकार दस्तावेजों, रजिस्टर और कई तरह के कागजातों का अंबार, भूमि के रखरखाव, परिवर्तन, वर्णन या परिभाषित करने के लिए चित्रगुप्त और यमराज के लेखे से कम नहीं थे। पटवारी कागजातों में ही दर्ज हो सकता था कि अमुक भूमि का मालिकी हक, कब्जा, विस्थापन, सरकारी स्वामित्व में ला दी गई भूमियों पर अतिक्रमण, जोत का अधिकार वगैरह शामिल माना जाए।
आदिवासी की खुद ईजाद की गई अर्थव्यवस्था में कई तत्वों का समावेश रहा है। इन सामूहिक गतिविधियों में शिकार करना, कृषि के लिए खेतों या क्षेत्र में परिवर्तन या अदल बदल भी करना, कुछ चुने हुए भूखंडों में स्वेच्छा से सामाजिक समझदारी के तहत खेती करना तथा पशुओं से संबंधित हर तरह की गतिविधि का लगातार उन्नयन करते रहना उसके अर्थशास्त्र के क्रमिक विकास के अलग अलग पड़ाव समझे जाते रहे हैं। गैरखेतिहर गतिविधियों में पेड़ों का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग, दोहन तथा निस्तार होता रहा है। राज्य द्वारा इस अर्थशास्त्र को अपने कानूनी तथा अधिनियमित तंत्र से जकड़कर एक तरह से अधिकारों की समझ पर ही डकैती कर दी गई। शुरू में तो यही लगा कि राज्य का अधिकार केवल प्रतीकात्मक तौर पर कायम करने के लिए रचा गया है। फिर दृश्य पर वन विभाग के अधिकारियों का प्रवेश और हस्तक्षेप होने लगा। शांत और स्वैच्छिक चले आ रहे आदिवासी अधिकारों में कटौती कर दी गई। परम्पराओं को नये प्रयोग के सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया जाने लगा। आदिवासियों में नया भावबोध उगा कि उनके जीवन के मुख्य लक्षण सामूहिकता को ही खत्म कर दिया जाना नया शगल या फितूर है। उन्हें मजबूर किया गया कि वे जंगल के उत्पादों और परिवेश का उपभोग और दोहन बहुत कम और जरूरी निजी हितों के लिए ही सरकारी नियंत्रण में रहकर कर सकेंगे।
राज्य ने उसे मुद्रा या करेंसी के आंकड़ों की अंकगणित में फंसाते आदिवासी जीवन के अहसास को ही एक तरह से विस्थापित कर नियंत्रित और संकुचित कर दिया। वन का उपभोग तथा प्रबंधन करने के नाम पर कड़े नियमों के जरिए आदिवास को ही जकड़ दिया गया। यह दबाव या हुक्म भी जारी किया गया कि आदिवासी वन अधिकारियों के स्वागत और उन्हें सुविधाएं देने के लिए कानूनबद्ध है। इसके एवज में उसे बतौर टोकन या कभी कभी तो पूूरी तौर से बेगार लेते अहसान से लाद दिया जाता। मानो उसका जीवन अब इन्हीं अनुभवों को महसूस करते रहने के लिए सरकार ने बंधक रख लिया है। सरकारी नियमों और अफसरों के दमन का एक असर और हुआ। उससे त्रस्त होकर कुछ आदिवासियों को यह विकल्प बेहतर और कारगर लगा कि वे और ज्यादा घने जंगलों की ओर पीछे हटते कूच करें जिससे सरकारी षड्यंत्र और आदेशों का कोड़ा उनकी पीठ पर न पड़े। वे उस परिवेश से उखड़ते रहे, जहां वे अपना पुश्तैनी आशियाना बनाए बैठे थे। घने जंगलों में नई बसाहट बनाने की मजबूरियों में उन्हें जीवनयापन के पहले से न्यूनतर साधनों पर गुजारा करने के लिए मजबूर होना पड़ने लगा।
व्यापारिक और औद्योगिक जरूरतों के कारण कुदरती जंगल काटे जाने लगे। पूंजीवाद के इस चेहरे ने सरकारी विधायन को ही अपना केचुल बनाकर उसमें प्रवेश किया। इसी कुटिलता ने आखिरकार अपने ही परिवेश और जीवन की चली आ रही सामूहिकता से आदिवासियों की बेदखली पूरी तौर पर सुनिश्चित कर दी। यदि वह रहना भी चाहता, तो उसे बरायनाम कुछ वेतन या पारिश्रमिक दिया जाकर अहसास कराया जाता कि वह अपने ही क्षेत्र की कुदरत का स्वामी रहा आने के बावजूद सरकारी व्यवस्था में बेबस बना दिया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में (स्वाभाविक ही) जनसंख्या का घनत्व बिरला होता है। इस वजह से व्यापारिक पैटर्न पर वन संपत्ति का दोहन शुरू करने के बाद सरकारों को बाहरी मजदूरों को लाने की जरूरत महसूस हुई। बाहरी मजदूरों को कुछ बेहतर वेतन या सेवा शर्तों के प्रलोभन के साथ साथ प्रभावित आदिवासी इलाकों में अस्थायी कारणों के बावजूद भविष्य की स्थितियों के लिए भी बसाहट की तरह रखी जाने लगी। अर्धशहरी क्षेत्रों या अन्य गांवों, कस्बों से लाए गए श्रमिकों का बेहद मासूम और भोले आदिवासियों से थोपा गया सामाजिक सहकार होने की नई परिघटना के कारण आदिवासियों को अपनी मानसिकता में कुंठा और घुटन होनी स्वयमेव महसूस होने लगी। यह जबरिया हस्तक्षेप सरकारों, कानूनों, पूंजीपतियों, नौकरशाहों और चुने हुए लेकिन निहित स्वार्थों के एजेन्ट बनते, लगते आदिवासी जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी पुष्पित, पल्ल्वित और पोषित होता रहा। वन विभाग के अधिकारी, प्रबंधक और निगम आदि के वनों के शोषक व्यापारियों के अलग अलग तरह के चेहरे और संस्करण ही रहे हैं। उन्हें पुलिसिया ताकतों से भी लैस किया जाने लगा।
अंगरेजी हुकूूमत के कठोर आदेशों के खिलाफ भारत के इतिहास में सबसे पहले और सबसे ज्यादा मर्दानगी का विद्रोह आदिवासियों ने ही किया है। उन्हें पूरी तौर पर कुचल दिये जाने या दबाये जाने का अहसास और भरोसा अंगरेज हाकिमों को नहीं होता था। फिर भी शोषण की प्रक्रिया बदस्तूर जारी रही। वन क्षेत्रों में लोकनिर्माण के कार्याे जैसे सड़क, पुल, भवन आदि बनाने में आदिवासियों को श्रमिकों के रूप में तब्दील किया जाना भी आवश्यक ही होता रहा। पारिश्रमिक बतौर धन का लालच देने पर भी आदिवासी मजदूर मुनासिब संख्या में काम करने नहीं आते थे। आदिवासी के लिए इस तरह से व्यापक तौर पर नियमित आदत बतौर नयी मूल्य व्यवस्था के तहत शराब पीना नया, निजी और फिर सामाजिक अनुभव बनाया जाता रहा। शहरी सभ्यता ने उनका मनोवैज्ञानिक शोषण करते शराबखोरी के जंगल में उन्हें धकेल दिया। आदिवासी के जीवन में स्वैच्छिक मदिरापान का अपना अनोखा सांस्कृतिक इतिहास और अहसास रहा है। उन्होंने उसे कभी भी उद्योग, व्यापार या सामाजिक दुर्गण नहीं समझा। पहले ब्रिटिश और बाद में भारतीय शहरी सभ्यता की कुटिल निगाहों से उसकी यह मासूम प्रथा भी विकृत की जाने लगी। एक आत्मनिर्भर मदिरा उपभोग की पारंपरिकता को सरकार और व्यवस्था पर निर्भर मदिरापान की नई साजिश में ढाल दिया जाए।
इस तरह आदिवासी समाज को धीरे धीरे कानूनतोड़क समाज में बदलता देखा जाने लगा। मदिरापान किए बिना न तो उसकी जरूरतें, परंपराएं और तीज त्यौहार सार्थक हो सकते थे। न ही वह ऐसे छोटे अपराध किए बिना अपनी मदिरा उपभोग की यथास्थिति कायम रख सकता था। आदिवासी के जीवन में सरकारी अपराधविज्ञान ने पूरी धमक के साथ अपने दखल की दस्तक दी। मुकदमे हजारों की संख्या में पैदा किए जाने लगे जिनका कोई औचित्य नहीं था। वे एक तरह से कैंसर की तरह भी उगाए गए।
शुरूआत में तो आदिवासी के उपचेतन की मानसिकता को सरकार द्वारा ईजाद की या थोपी गई अधिकार हस्तक्षेप की परिघटना असुविधाजनक लगने के बावजूद आपत्तिजनक नहीं लगी। तब तक उसने भी जीवनयापन के लिए उपलब्ध होते रहे सभी तरह के वनउत्पादों के कारण शाल वृक्षों की कटाई को किसी खतरे की घंटी नहीं समझा था। जंगल से आध्यात्मिक तथा मनोवैज्ञानिक रोमांस आदिवासी का सदियों पुराना रोमांचकारी अनुभव रहा है। वह अनुभव धीरे धीरे एक तरह की जीवन-अनुभूति में बदल चुका था। जीवन से ऐसी आंतरिक संगति उसे प्राकृतिक वन-संगीत की सिम्फनी से लबरेज रखती थी। वह आत्मतुष्ट स्वाभाविक जीवन पद्धति का आदी हो चुका था। जंगल उसके जीवन में एक तरह का एडवेंचर, उन्माद, उत्साह और उत्फुल्लता का स्वाभाविक और बुनियादी कारक रहे हैं। उसका यह अहसास आज तक कायम है। सरकारी स्तर पर ठूंस दी गई व्यापारिक नस्ल की शराबखोरी आदिवास के जीवन में बहुत घातक और परिवतर्नकारी हस्तक्षेप होती गई है। वनों का विनाश और ठेकेदारी के जरिए उसका व्यापारीकरण साहूकारों के साथ गलबहियां कर आदिवासी जीवन को उसे नष्ट करने के लिए कैंसर की तरह उगाई गई प्रवृत्तियां ही समझी जा सकती हैं।
नए तरह के तत्व और व्यक्ति आदिवासी जीवन में हस्तक्षेप, प्रयोग, परिवर्तन या प्रोन्नति के नाम पर आए या भेजे गए। जनजातियों को मजबूर किया गया कि अपनी खेतिहर उपजें और कुदरती वन उत्पाद बाजार नामक नई व्यावसायिक एजेंसी को ऐसी दरों पर बेचने के लिए मजबूर हों जिन्हें सरकार और बाजार ने अपने अधिकारों के जरिए खरीदने के लिए तय किया है। आदिवासी तो क्या शहरी नागरिक जीवन को भी कभी समझ नहीं आ पाया कि ऋणग्रस्तता कितना बड़ा स्थायी अभिशाप और किस तरह है। कर्ज में लिये मूल धन की ब्याज सहित अदायगी के बावजूद वह कैसा चक्रवृद्धि ब्याज है जो कर्जदार की गर्दन पर फांसी के फंदे की तरह जल्लाद साहूकारों के हाथों में हर वक्त मचलता रहता है। ऐसे भयावह शोषण की हालत में धीरे धीरे अपने कृषि और वनोपज से वंचित होता, शराबखोरी और ऋणग्रस्तता में जकड़ा जाता आदिवासी समाज उन आधारभूत संरचनाओं तक को बेच देने तक के लिए लाचार कर दिया गया जो उसके जीवनयापन की ही बुनियाद रही हैं। स्त्रियों के शील और सम्मान के प्रति चरित्रवान रहा आदिवासी समाज कथित सभ्य लोगों के कुटैव के कारण उनसे ही स्त्रियों के शील की रक्षा कर पाने में लाचार होना भी महसूस करता रहा। धीरे धीरे उसमें यह मानसिकता तपेदिक के बीमार की तरह घर करती गई कि वह दिखने में तो आदिवासी परंपराओं से संपृक्त लगता अपने अतीत का वर्तमान है, लेकिन दरअसल उसे अपनी स्वायत्तता, इयत्ता, पहचान और प्रकृति से तादात्म्य को लगभग पूरी तौर पर खो देना पड़ा है।
प्रकृतिसम्पन्न जीवन-स्वायत्त आदिवासी धीरे धीरे आर्थिक पैमानों पर गरीब होता चला गया। उसकी कृषि भूमियां भी उससे छीनी जाने लगीं। जिन वनोत्पादों पर वह निर्भर था, वे भी उससे जबरिया खरीद लिए जाते रहे। शहरी सभ्यता का आदिवासी जीवन से पूरी तौर पर अजनबीपन, अपरिचय और अलगाव रहने से उस कथित आर्य नागर जीवन का प्रत्यक्ष आक्रमण वन संस्कृति पर नहीं हुआ था। अछूत या दलित वर्ग की सामाजिक संरचना और जीवनानुभव लेकिन उच्च वर्गों से दैनिक सहकार के साथ अलगाव की मनोवैज्ञानिक स्थितियों के ठहराव के लिए सदियों का समय लगा था। वनों में गैरआदिवासी वर्गसमूह शासक, ठेकेदार, व्यापारी या अन्य चेहरों और चोचलों में पहुंचा। वह अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता, सियासी हुनर, आर्थिक तंत्र और व्यापारिक कुटिलता के चलते प्रकृति के सभी स्त्रोतों पर कब्जा जमाता वनों के परिवेश में नया वर्चस्वकारी शासक वर्ग बनता गया। इस वर्ग का शहरी सभ्यता, सरकार, नौकरशाहों, आधुनिक प्रविधियों और उन सब जीवन संसाधनों से सरोकार था जो उसे लगातार समृद्ध बनाते रह सकते थे। सरकार ने तथाकथित कानूनों की रचना के माध्यम से गैरकुलशील समझे जाते अशिक्षित, निरक्षर, मासूम और सीधे साधे आदिवासियों को कानूनी व्यवस्थाओं में जकड़कर इतना लाचार कर दिया कि क्रूर, कुटिल और कथित कुलशील आक्रामकों ने बहुत तेजी से उनकी बर्बादी का दस्तूर कायम रखा।
यह सब अब तो भारत के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को बेहद तकलीफ के साथ झेलना पड़ रहा है। सरकारी व्यवस्था पर निर्भर होकर उन्हें अपने स्वामित्व से वंचित होकर किराएदार या लाइसेंसधारी बनाने का अजीबोगरीब प्रयोग किया गया है। शिक्षा और आधुनिक समझ से वंचित होने के कारण आदिवासी की बहुमूल्य संपत्तियां औने पौने और बरायेनाम दरों पर खरीदी जाने लगीं। मसलन उसके कब्जे का एक पेड़ काटकर उसे इतने कम मूल्य पर बेचने की समझाइश का कुचक्र रचा गया, मानो वह पेड़ उसके जीवन और अस्तित्व की अतिरिक्तता रहा हो। लकड़ी का एक टुकड़ा भी खेती के लिए हल बनाने के लिए यदि वह काट लेता, तो उसे जंगल विभाग के जंगली कानून वन उत्पाद की चोरी के आरोप में अपनी गिरफ्त में लेकर मुलजिम बनाकर उसका दमन और शोषण करते रहे। यदि वह विरोध करता तो उसे वन अधिनियम के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता के क्रूर कानूनों में परिभाषित कथित अपराधों के चंगुल में गिरफ्तार कर जेलों में ठूंस दिया जाने लगा। वहां से जमानत के अभाव में उसका छूटना लगभग असंभव होता रहा। फिर तो यह भी होता रहा कि निर्धारित अधिकतम सजा की अवधि के बाद भी आदिवासी का जेल से छूटना उसके अज्ञान, अशिक्षा और गरीबी के कारण उसके जीवन प्रारब्ध का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाने लगा। बहुत कम संख्या में गैरआदिवासियों के कुछ मानव अधिकार संगठनों के अपवादों को छोड़कर सभ्यता, सरकार और समाजचेता व्यक्तियों से आदिवासियों को अपेक्षित सहायता मिलने का कोई उत्साहजनक या गौरवपूर्ण इतिहास-अनुभव पढ़ने में नहीं आता।
किताबी ज्ञान की तुलना में दुनियावी और प्राकृतिक स्त्रोतों से प्राप्त अनुभव ज्यादा प्रामाणिक होता है। यही तो आदिवास के जीवन ने साक्षर नागर समाज को लगातार अहसास कराया है। विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में सरकारों द्वारा जितने भी प्रोजेक्ट, परियोजनाएं और प्रयोग किए गए, उनमें पहले यह सम्यक परीक्षण नहीं किया गया कि वन जीवन की सभी बारीकियों से ऐसे अभिनव अभियान की कितनी और कब तक सुसंगति बैठ सकती है। कई बार ऐसे कार्यक्रम परिणामधर्मी और युगांतरकारी दिखते भर रहे, लेकिन उनमें खर्च की गई धनराशि के अनुपात में उपलब्धि का आंकड़ा लचर या सिफर ही रहा है। ऐसी भी परियोजनाएं लाई जाती रहीं जिनमें व्यय होने वाला शासकीय भार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आदिवासियों या उनके क्षेत्रों पर करारोपण के जरिए वसूल भी किया जाता रहा। आदिवासी तो क्या साक्षर व्यक्ति को भी पता नहीं होता कि वह क्यों और कैसे दस्तावेज पर अपना हस्ताक्षर या अंगूठा किन विपत्तियों को संभावित तौर पर आमंत्रित करने के लिए लगाने अभिशप्त है। फितरतें सरकारी योजनाओं को लगातार असफल करती ऐसे ढर्रे पर आ खड़ी हुई हैं जिन्हें सुधार पाना सरकारों के लिए अब संभव होता भी नहीं दिख रहा है। इसका फौरी दुष्परिणाम आदिवासी इलाकों में सरलता से देखने में आता है।
सरकारें हैं कि मासूम आदिवासियों की लूट के इस जश्न में अब तक लगातार जश्नजूं हैं। प्रशासनिक तंत्र में अधिक आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और तकनालाॅजी का उद्भव और विकास हो गया है। वह तो औसत साक्षर नागरिकों तक को भी समझ नहीं आता। उस वजह से आदिवासी इलाकों में तो कथित हितग्राहियों को अपने अधिकारों से ज्यादा तेजी से च्युत होना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में विधायिका महत्वपूर्ण विधि उत्पादक संस्था है। आजादी के बाद केन्द्र और राज्य के स्तर पर इतनी अधिक संख्या में नए अधिनियमों का विधायन और पुराने अधिनियमों में संशोधन किया जाता रहा है कि अदालतें और वकील भी कानून की बारीकियों पर सही जगह उंगली नहीं रख पाते। इन सब बातों का खामियाजा बिना किसी प्रतिभागिता किए भी आदिवासियों को सबसे ज्यादा झेलना तो पड़ रहा है।
कई सरकारी अधिकारी आदिवासी क्षेत्रों में पदस्थापना से बचने के बावजूद स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तब वे नियोक्ता के प्रति उपजी अपनी प्रतिहिंसा का बदला आदिवासी समस्याओं के निदान करने में भुनाते रहते हैं। उनकी प्राथमिकता हर वक्त यही होती है कि जैसे भी हो उन्हें काला पानी के उस इलाके से स्थानान्तरित कर उनके वांछित शहरों में भेज दिया जाए। यह सोच, प्रकल्प और उद्यम यदि नीयतन ठीक भी हो तब भी अपनी प्रक्रियात्मक खोट के कारण उस छुरी की तरह है जो आदिवास के जीवन अहसास के खरबूजे पर उसे काटने के लिए ही गिरती है।
सदियों से आदिवासियों का इत्मीनान भी रहा है कि वे नागर सभ्यता के पूरक हैं, उसके अधीन या उससे कमतर नहीं। सदियों से नागर सभ्यता और सामंती शासन से दूर, मुक्त और निरपेक्ष रहे वन क्षेत्र प्राकृतिक संपदा से भरपूर होने के कारण सत्ता की लोलुपता के स्वाभाविक शिकार बने। तरह तरह के खनिज पदार्थ और वन उत्पाद उनमें सत्ताभिमुख महत्वाकांक्षाएं उगाते रहे कि बड़ी सिंचाई योजनाएं, विद्युत उत्पादन प्रकल्प और खनिज आधारित उद्योग लगाने के लिए वन क्षेत्र मानो उनके लिए इतिहास ने सदियों से सुरक्षित रखे थे। चपल, कुटिल और विरल बुद्धि के ब्रिटिश शासकों ने ऐसी तमाम परियोजनाओं को लगाने में अपनी तरफ से देर नहीं की। मशीनी सभ्यता का यह एक तरह से भारत के लिए अभिशाप और भविष्य के भारत के लिए वरदान भी रहा कि वह अपनी आजादी के बाद उसे प्राप्त और उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञान और अनुभव से किस तरह अपनी आर्थिक संरचना को चुस्तदुरुस्त करे। ब्रिटेन की औद्योगिक हविश के चलते आदिवासी इलाकों में पारंपरिक प्रविधियों के लिए कोई विकल्प शेष नहीं बचा। आदिवासियों और अन्य श्रमिकों का सभ्यता के प्रतिमानों पर लगातार हाशियाकरण होता रहा। वह स्थिति स्वतंत्रता के सत्तर वर्ष बाद भी जस की तस बिना थके अट्टहास कर रही है।
जितने भी आर्थिक, औद्योगिक और अन्य प्रकल्प शासकीय फाइलों में उपजते हैं, उनके किताबी ज्ञान में जमीनी हकीकत का संदर्भ काल्पनिक तो हो सकता है। वह आदिवासी परिवेश में ठहरी हुई सचाइयों से मुठभेड़ कर ही नहीं सकता। रूबरू भी नहीं होना चाहता। उसे अपनी किसी भी परियोजना के लिए आदिवासियों के सांस्कृतिक, मानवीय, तकनीकी और अनुभवसिद्ध कौशल की आवश्यकता महसूस नहीं होती। वह उन्हें केवल श्रमिक, कृषक या बेगार करने वाला कर्मी मानने के अतिरिक्त अपने प्रकल्पों को मनुष्य आधारित बनाने से परहेज करता है। इसकी भी पृष्ठभूमि में नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों के साथ काॅरपोरेटी गठजोड़ की युति होती है। आदिवासी क्षेत्र तो केवल संदर्भ की तरह इस्तेमाल होते हैं। वजह यह है कि उनके ही पास धरती के नीचे हर तरह के खनिज और धरती के ऊपर हर तरह के वनोत्पाद और धरती पर सबसे सस्ती दरों पर अकुशल श्रमिक उपलब्ध होते हैं। इन सरकारी योजनाओं में एक और आग्रह है। अपना त्वरित लाभ प्राप्त करने के लिए नेता- नौकशाह-काॅरपोरेट गठजोड़ बहुत तेज गति से विकास करने का मुखौटा लगाए है। वह अपने आर्थिक लाभ का सपना साकार कर लेना चाहता है। ऐसा आर्थिक लाभ वह भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता। तेज गति होने के कारण आदिवासी वृत्ति का सहकार नहीं हो पाता। इसलिए वह ऐसी परियोजनाओं में भागीदारी या सेवा करने के लिए बुलाया जाने पर भी झिझकता रहता है।
औद्योगिक, खनिज, सिंचाई और विद्युत प्रोजेक्ट आदिवासियों की छातियों पर ही अमूमन उगाए गए हैं, लेकिन ‘दिया तले अंधेरा‘ जैसी कहावत को चरितार्थ करते उन प्रकल्पों का सीधा लाभ उन्हें नहीं मिल पाया। अंगेजों के बनाए बदनाम भू अर्जन अधिनियम 1984 के तहत स्वेच्छया या जबरिया अर्जित भूमि का इतना कम मुआवजा दिया जाने लगा जो प्रभावित आदिवासी को मजबूर करता कि वह अपने प्रभावित परिवेश से विस्थापित होने पर लगभग मुफलिसी की जिंदगी जीने के लिए खुद ही विकल्प ढूंढे। उसका जीवन बूर्जुआ नौकरशाही की समझ और साम्राज्यवादी उद्योगधर्मिता के चारों और चकरघिन्नी की तरह घूमते रहने को मानो प्रतिशोधित किया गया। बरायनाम मिला क्षतिपूर्ति का धन आदिवासी से लूट लेने के लिए शराब ठेकेदार और साहूकार की उपस्थिति शासन ने पहले ही सुनिश्चित और स्थापित कर रखी थी। इस तरह एक सुरचित जीवन श्रृंखला अस्तित्वहीन नामालूम इकाइयों में सरकारी कुसमझ बल्कि षड़यंत्र के कारण बदलते रहने को भी आदिवासी जीवन कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र स्थानापन्न किए जाते आदिवासियों को लगातर विपन्न बना रहा है। इसके बाद भी देश के कर्णधार कथित आर्थिक सूचकांक को संपन्न होने का प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं। एक सुगठित समाज यदि इकाइयों में टूट रहा है, तो उससे भी तो भारतीय सामाजिक संरचना को ही नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।