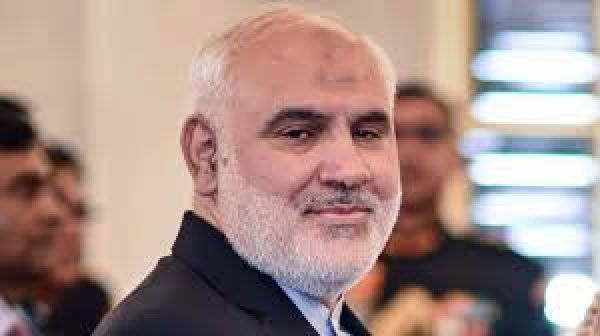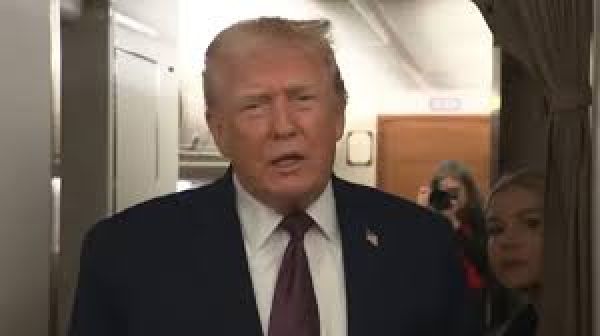अंतरराष्ट्रीय

इस महीने की शुरुआत में वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने एक जनमत संग्रह करवाया.
इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें पड़ोसी देश गुयाना के एसेकिबो क्षेत्र का वेनेज़ुएला में विलय करने का अधिकार प्राप्त हो गया है.
यह दो सौ साल पुराने भूमि विवाद में आया नया मोड़ है. इसमें एक तरफ़ तीन करोड़ की आबादी वाला विशाल देश वेनेज़ुएला है और दूसरी तरफ़ दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर बसा गुयाना है. गुयाना की आबादी केवल आठ लाख है.
गुयाना ने कहा है कि वो अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा.
वहीं वेनेज़ुएला के पड़ोसी देशों और विश्व के कई दूसरे देशों ने भी राष्ट्रपति मादुरो से कहा है कि वो कोई आक्रामक कदम ना उठाएं. मगर अब तक मादुरो ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की अपील को नज़रअंदाज़ ही किया है.वहीं वेनेज़ुएला के पड़ोसी देशों और विश्व के कई दूसरे देशों ने भी राष्ट्रपति मादुरो से कहा है कि वो कोई आक्रामक कदम ना उठाएं. मगर अब तक मादुरो ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की अपील को नज़रअंदाज़ ही किया है.
एसेकिबो क्षेत्र
एसेकिबो क्षेत्र गुयाना के दो-तिहाई क्षेत्र में फैला हुआ है. यानि इसका क्षेत्रफल अमेरिका के फ़्लोरिडा राज्य के बराबर है. पहाड़ी वर्षा वनों के इस क्षेत्र की सीमा वेनेज़ुएला से जुड़ी है.
इसके महत्व पर हमने बात की फ़िल गनसन से जो इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में वरिष्ठ विश्लेषक हैं. हमने उनसे जानना चाहा कि वेनेज़ुएला ने पहली बार कब इस क्षेत्र पर दावा किया?
वो कहते हैं, ''यह विवाद उपनिवेश काल में शुरू हुआ था. इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि स्पेन के उपनिवेशियों ने एसेकिबो क्षेत्र पर कब्ज़ा किया हो. मगर उनके नक़्शों में दिखाया गया था कि वेनेज़ुएला के नौसेना प्रमुख एसेकिबो नदी तक पहुंचे थे. इसी के आधार पर वेनेज़ुएला ने एसेकिबो क्षेत्र पर दावा किया था.''
सैद्धांतिक रूप से तो यह विवाद 1899 में हल हो गया था, जब पेरिस में पांच अंतरराष्ट्रीय जजों ने इस पर अपना फ़ैसला सुनाया था. जजों की इस पीठ में दो ब्रितानी, दो अमेरिकी और एक रूसी जज शामिल थे. इन जजों ने एसेकिबो क्षेत्र का स्वामित्व ब्रिटिश गुयाना को सौंप दिया था. वेनेज़ुएला को कुछ नहीं मिला. उस समय वेनेज़ुएला ने अनमने तरीके से फ़ैसला मान लिया था.
लेकिन बाद में उसे लगा कि अंतरराष्ट्रीय जजों ने आपस में मिल कर उसे उसके अधिकार से वंचित कर दिया. उसके इस संदेह को तब और बल मिला जब 1949 में उस अदालत के एक अधिकारी द्वारा तैयार किए गए समझौते का मसौदा सामने आया.
फ़िल गनसन ने बताया, ''समझौते के मसौदे में लिखा गया था कि ब्रितानी और रूसी जज ने मिल कर अमेरिकी जजों के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो इसे नहीं मानेंगे तो फ़ैसला और प्रतिकूल बना दिया जाएगा.''
यह बात सामने आने के बाद वेनेज़ुएला की क्या प्रतिक्रिया थी?
फ़िल गनसन कहते हैं, ''वेनेज़ुएला ने फ़ैसले को चुनौती दी और संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगाई. मगर उसे कुछ ख़ास हासिल नहीं हुआ. अंतत: 1966 में जेनेवा समझौता हुआ. आज भी राष्ट्रपति मादुरो की यही दलील है कि इस विवाद का समधान उसी अदालत में हो.''
उस समय गुयाना आज़ाद होने जा रहा था लेकिन वेनेज़ुएला के साथ एसेकिबो के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो पाया. जब ह्यूगो शावेज़ 1999 में वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया. समझा जाता है कि उन्होंने ऐसा अपने सहयोगी और क्यूबा के नेता फ़िदेल कास्त्रो की सलाह पर किया.
फ़िल गनसन का कहना है कि कास्त्रो ने शावेज़ के सामने यह दलील रखी कि अगर वो कैरेबियाई देशों और अन्य देशों का समर्थन चाहते हैं तो उन्हें एसेकिबो पर अपने दावे को छोड़ना पड़ेगा.
मगर मादुरो के वेनेज़ुएला में सत्ता में आने के दो साल बाद 2015 में गुयाना में एसेकिबो के तट के पास पानी के नीचे बड़े तेल भंडार की खोज हुई. इससे स्थिति बदल गई. वेनेज़ुएला के लिए एसेकिबो का महत्व बढ़ गया.
2018 में संयुक्त राष्ट्र की सिफ़ारिश पर यह मामला दी हैग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहुंच गया, लेकिन वेनेज़ुएला का कहना है कि यह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. आख़िर वेनेजुएला अंतरराष्ट्रीय न्यायलय द्वारा मामले की सुनवाई का विरोध क्यों कर रहा है?
फ़िल गनसन की राय है, ''शायद एक वजह यह है कि वेनेज़ुएला को लगता है कि वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा हार जाएगा. लेकिन मुझे लगता है कि वो इस मुद्दे को ज़िंदा रखना चाहते हैं ताकि इसके बल पर देश की घरेलू राजनीति में राष्ट्रवादी भावनाओं को हवा दी जा सके. निकोलस मादुरो के रवैये को देखते हुए तो यही लगता है.''
वेनेज़ुएला इस मामले में अगला कदम क्या उठाएगा यह एक व्यक्ति पर निर्भर करता है.
राष्ट्रपति निकोलस मादुरो
न्यू यॉर्क यूनिवर्सिटी में आधुनिक लातिन अमेरिकी इतिहास के प्रोफ़ेसर अलेहांड्रो वेलेस्को कहते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज़ ने निकोलस मादुरो को अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन वो जनता के बीच शावेज़ की तरह लोकप्रिय नहीं थे.
वो कहते हैं, ''मादुरो काफ़ी छोटे अंतर से चुनाव जीते थे. सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की बली चढ़ा दी. विरोध प्रदर्शनों को कुचल दिया और फ़र्ज़ी चुनाव करवाए.''
मादुरो की राजनीतिक विचारधारा क्या है?
इस सवाल पर अलेहांड्रो वेलेस्को कहते हैं, ''ज़ाहिर है कि वो शावेज़ के उत्तराधिकारी हैं और समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे हैं लेकिन उनकी नीतियों में कई असंगितयां और विरोधाभास नज़र आता है. वैसे तो वो अमेरिकी साम्राज्यवाद के विरोध की बात करते हैं लेकिन अन्य जगहों पर साम्राज्यवाद का समर्थन करने में नहीं हिचकिचाते. एक तरफ़ वो डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था का विरोध करते रहे हैं और दूसरी ओर उन्होंने वेनेज़ुएला की अर्थव्यवस्था को डॉलर पर आधारित कर दिया.''
उनके सत्ता में आने के बाद वेनेज़ुएला की अर्थव्यवस्था कैसी रही है?
इस सवाल पर अलेहांड्रो वेलेस्को के अनुसार पिछले दस सालों में अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर हो गई है जितनी लातिनी अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं हुई थी. महंगाई आसमान छू रही है और मुद्रास्फिती की दर दो हज़ार प्रतिशत तक पहुंच गई है. बिजली उत्पादन व्यवस्था ठप्प होने की कगार पर है. हर दिन बिजली कटौती होती है. खाद्य सामग्री से लेकर दवाइयां तक आयात हो रही हैं. महंगाई से तंग आ कर पिछले दस सालों में सत्तर लाख से अधिक लोग देश छोड़ चुके हैं.
अलेहांड्रो वेलेस्को का कहना है कि अर्थव्यवस्था के गिरने का एक कारण वेनेज़ुएला की तेल निर्यात पर अत्याधिक निर्भरता भी है.
वो कहते हैं, ''तेल उद्योग के कुप्रबंधन की वजह से वेनेज़ुएला की अर्थव्यवस्था ढह गई है. अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमत भी गिरी है. दूसरी वजह यह है कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला के ख़िलाफ़ कई प्रतिबंध लगा रखे है.''
यही वजह है कि वेनेज़ुएला ने एसेकिबो में तेल भंडारों की खोज के बाद उस पर अपने दावे को फिर से सामने रख दिया है और देश में एसेकिबो के संबंध में जनमत संग्रह कराया गया. जनमत संग्रह में जनता के सामने पांच सवाल रखे गए जिसमें उन्हें हां या ना के पक्ष मे वोट देना था.
जनता के सामने सवाल थे कि क्या एसेकिबो विवाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है. दूसरा सवाल था कि क्या एसेकिबो का एक नए राज्य के रूप मे वेनेज़ुएला में विलय होना चाहिए? 95 प्रतिशत जनता ने सभी सवालों का जवाब हां में दिया.
अलेहांड्रो वेलेस्को को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उनके अनुसार एसेकिबो पर देश का दावा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर देश की सभी विचारधारा के लोग एकजुट हैं. अब देखना यह है कि एसेकिबो पर अपने दावे के लिए वो अगला कदम क्या उठाते हैं और गुयाना और अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसके जवाब मे क्या कार्रवाई करता है.
गुयाना और वेनेज़ुएला के दोस्त
लंदन स्थित चैटहैम हाउस में वरिष्ठ शोधकर्ता डॉक्टर क्रिस्टोफ़र सबातिनी कहते हैं कि आठ लाख की आबादी वाले गुयाना में ग्यारह अरब बैरल की मात्रा में तेल की खोज हुई है. इस तेल भंडार ने गुयाना का भाग्य बदल दिया है.
वो कहते हैं, ''2020 में गुयाना की जीडीपी यानि सकल घरेलू उत्पाद में 80 प्रतिशत वृद्धि हुई. वह दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है. देश के ख़ज़ाने में पैसे तो आ रहे हैं लेकिन जनता यह भी सोच रही है कि यह खर्च किस पर होंगे.''
यह धन कहां खर्च होगा इसका फ़ैसला गुयाना के राष्ट्रपति इरफ़ान अली को करना है, मगर फ़िलहाल उनका ध्यान वेनेज़ुएला की चुनौती से निपटने पर है. वो 2020 में विवादास्पद चुनावों के बात सत्ता में आए थे.
क्रिस्टोफ़र सबातिनी ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति के ख़िलाफ़ अविश्वास मत पारित होने के बाद चुनाव हुए. मगर उन्होंने शुरुआत में चुनाव के नतीजे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. चुनाव के कई हफ़्तों बाद वो सत्ता से हटे. मगर दो प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच मतभेद बरकरार है, जो गुयाना के नस्लीय समीकरणों को भी प्रभावित कर रहा है.
सत्तारुढ़ पार्टी का झुकाव अफ़्रीकी मूल के लोगों की तरफ़ है जबकि दूसरे दल का प्रभाव दक्षिण एशियाई मूल के लोगों पर अधिक है.
गुयाना की जनता, ख़ास तौर पर एसेकिबो के लोग इस मुद्दे पर एकजुट हैं कि यह क्षेत्र गुयाना का हिस्सा बना रहे. कुछ अनुमानों के अनुसार एसेकिबो की आबादी एक-दो लाख के बीच है.
गुयाना के राष्ट्रपति इरफ़ान अली फ़िलहाल वेनेज़ुएला के साथ विवाद में कूटनीति का रास्ता अपना रहे हैं. उन्होंने कई तेल कंपनियों को गुयाना के तेल भंडारों से तेल निकालने के लिए आमंत्रित किया है.
इसके साथ ही वो कैरेबियाई देशों, ब्रिटेन और चीन से भी इस मामले में सहायता चाहते हैं. उन्होंने चीन को भी एसेकिबो से तेल निकालने और देश में विकास के कई प्रोजेक्ट में शामिल किया है. इस बात से वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति मादुरो नाराज़ हैं क्योंकि चीन वेनेज़ुएला का सहयोगी देश रहा है.
चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य भी है. हाल में गुयाना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हस्तक्षेप करने की अपील करते हुए कहा है कि वेनेज़ुएला गुयाना पर हमला कर सकता है. मगर रूस भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है और वेनेज़ुएला का सहयोगी है.
क्रिस्टोफ़र सबातिनी का कहना है, ''रूस का मामला अलग है. ना कि रूस के वेनेज़ुएला के साथ घनिष्ठ संबंध हैं बल्कि वेनेज़ुएला के तेल उद्योग में उसकी बड़ी हिस्सेदारी है. इसलिए रूस के आर्थिक और राजनीतिक हित वेनेज़ुएला के साथ जुड़े हुए हैं.''
विवाद पर दुनिया की नज़र
ऑक्सफ़र्ड यूनिवर्सिटी के ब्लावाटनिक स्कूल ऑफ़ गवर्नमेंट की प्रोफ़ेसर और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर एनेटा इडलर का मानना है कि वेनेज़ुएला के पड़ोसी देश ब्राज़ील समेत विश्व के कई देश और अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं चाहते कि लातिन अमेरिका में संघर्ष शुरू हो.
''ब्राज़ील की सीमा वेनेज़ुएला और गुयाना से सटी हुई है. ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा ने वेनेज़ुएला से समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील की है मगर अपनी सेना को उत्तरी सीमा पर तैनात भी कर दिया है."
वो कहती हैं, ''कैरेबियाई देशों के संगठन कैरिकॉम और राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के संगठन ने भी वक्तव्य जारी कर के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिसंबर में जारी की गई उस अपील को दोहराया है जिसमें कहा गया था कि अदालत का फ़ैसला आने से पहले वेनेज़ुएला कोई कार्रवाई ना करे. इसके बावजूद कुछ ही दिनों बाद वेनेज़ुएला ने इस मुद्दे पर जनमत संग्रह करवा लिया.''
डॉक्टर एनेटा इडलर की राय है कि इस विवाद को सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती.
डॉक्टर एनेटा इडलर कहती हैं कि इसकी वजह यह है कि एक तरफ़ अमेरिका और यूके हैं, जो काफ़ी हद तक गुयाना के पक्ष में हैं. दूसरी तरफ़ चीन और रूस हैं और रूस वेनज़ुएला का करीबी सहयोगी है. इसका मतलब यह है कि सुरक्षा परिषद में ऐसा प्रस्ताव पारित होना मुश्किल है जिस पर पांचों स्थायी सदस्य देश एकमत हों.
विगत में मादुरो पर अंतरराष्ट्रीय दबाव का ख़ास असर नहीं पड़ा है. अगर मादुरो गुयाना पर हमला कर देते हैं तो क्या हो सकता है?
इस सवाल पर डॉक्टर एनेटा इडलर कहती हैं कि सैन्य क्षमता में दोनों देशों के बीच कोई बराबरी नहीं है. वेनज़ुएला के पास लगभग साढ़े तीन लाख सैनिक और भारी हथियार हैं, जबकि गुयाना के पास केवल चार हज़ार सैनिक हैं. मगर वेनेज़ुएला अगर हमला करता है तो अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी. क्योंकि 2015 में अमेरिकी कंपनी एक्सॉनमोबील ने एसेकिबो क्षेत्र में तेल भंडारों की खोज की थी.
डॉक्टर एनेटा इडलर ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के प्रवक्ता ने पहले ही मौजूदा स्थिति को चिंताजनक करार दिया है. अमेरिकी नौसेना के दक्षिणी कमांड ने गुयाना में हवाई निगरानी उड़ान भरना शुरू कर दिया है. हालांकि उसका कहना है अमेरिका और गुयाना के बीच सुरक्षा संबंधों के तहत यह एक सामान्य कार्रवाई है. मगर यह एक महत्वपूर्ण कदम है.
अगर अमेरिका गुयाना के समर्थन में हस्तक्षेप करता है तो वेनेज़ुएला के सहयोगी देश रूस और चीन की क्या प्रतिक्रिया होगी?
डॉक्टर एनेटा इडलर के अनुसार ऐसा हुआ तो शीत युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी. उस दौरान भी लातिन अमेरिका संघर्ष का केंद्र बनने की कगार पर था.
तो अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न की ओर- क्या वेनेज़ुएला अपने पड़ोसी पर हमला करने वाला है? वहां स्थिति तेज़ी से बदल रही है.
कुछ सप्ताह पहले तक लोग सोच रहे थे कि मादुरो जनमत संग्रह करवा के संतुष्ट हो जाएंगे. लेकिन उसके बाद उन्होंने वेनेज़ुएला की सरकारी तेल कंपनी को निर्देश दिया है कि एसेकिबो क्षेत्र से तेल निकालने के लिए लाइसेंस जारी करे.
उन्होंने एक नक़्शा जारी किया जिसमें एसेकिबो को वेनेज़ुएला में विलीन हुए नए राज्य के तौर पर दिखाया गया है. उन्होंने घोषणा की कि एसेकिबो क्षेत्र के निवासियों को वेनेज़ुएला के पहचान पत्र दिए जाएंगे. अगर उन्होंने गुयाना पर हमला किया तो उन्हें भारी अंतरराष्ट्रीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा.
वहीं कुछ दिन पहले बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में गुयाना के राष्ट्रपति अली ने कहा कि अगर गुयाना को कुचलने की कोशिश की गई तो उसके मित्र देश हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे.
गुयाना के सहयोगी देश अमेरिका की सेना पहले ही क्षेत्र में मौजूद है. उम्मीद की जा रही है कि इस सप्ताह राष्ट्रपति मादुरो और राष्ट्रपति अली के बीच सेंट विनसेंट में होने वाली वार्ता से स्थिति को शांत करने में मदद मिलेगी. लेकिन हमने पिछले दस सालों में यही देखा है कि वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति मादुरो अगला कदम क्या उठाएंगे इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है. (bbc.com)