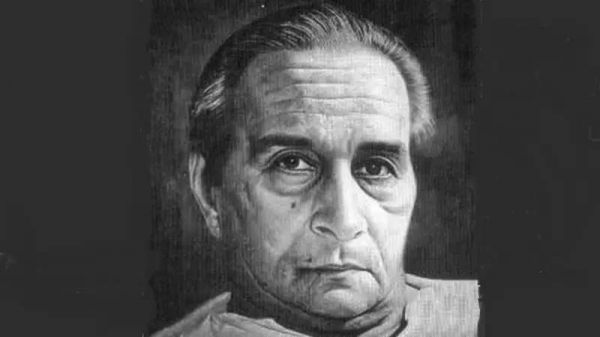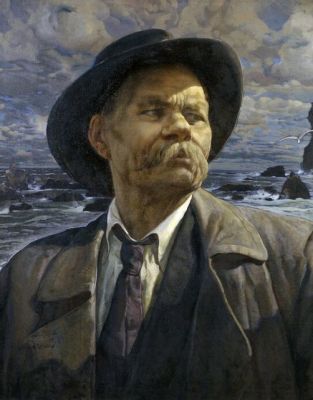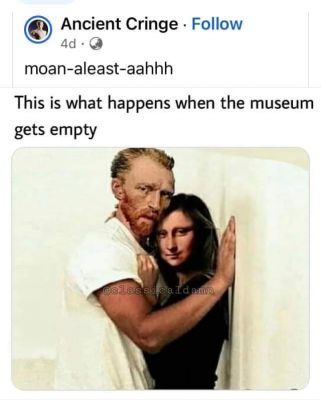विचार/लेख
शेख हसीना के हाथ से बांग्लादेश की सत्ता निकले एक महीना हो गया है।
बीते दिनों ऐसे कई वाकय़े रहे, जिसमें बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार समेत अहम पक्षों ने पाकिस्तान और चीन से रिश्ते मज़बूत करने के संकेत दिए हैं।
एक महीने पहले तक जो बांग्लादेश भारत के करीब था, वो अब चीन और पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की वकालत कर रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैय्यद अहमद ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मंत्री नाहिद इस्लाम से एक सितंबर को मुलाकात की थी।
अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाईम्स ने एक अधिकारी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नाहिद इस्लाम ने इस मुलाकात में पाकिस्तान के साथ 1971 का मसला सुलझाने की बात की। दोनों देशों के बीच बीते सालों में 1971 की लड़ाई एक अहम मुद्दा रही है।
इससे पहले 30 अगस्त को पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से बात की थी।
चीन की पहल
1971 में पूर्वी पाकिस्तान जंग के बाद पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश के बनने में भारत की अहम भूमिका थी। वहीं चीन बांग्लादेश बनाए जाने के खिलाफ था।
मगर अब बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार चीन की ओर कदम बढ़ाती दिख रही है।
कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी पर लगी पाबंदी हटाई गई थी। जमात-ए-इस्लामी पर शेख़ हसीना सरकार ने 2013 में पाबंदी लगाई थी।
जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी है। इस पार्टी का छात्र संगठन काफ़ी मज़बूत है। जिस आंदोलन के बाद शेख़ हसीना की सत्ता गई, उसमें इस संगठन के छात्रों की भूमिका अहम रही है।
इस पर देश में हिंसा और चरमपंथ को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं।
भारत में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जमात पर बांग्लादेश में हिन्दू विरोधी दंगे भडक़ाने का भी आरोप लगा था। जमात-ए-इस्लामी की छवि भारत विरोधी मानी जाती है।
जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफीक-उर रहमान ने बीते दिनों कहा था- भारत ने अतीत में कुछ ऐसे काम किए हैं जो बांग्लादेश के लोगों को पसंद नहीं आए।
शफीक-उर रहमान ने बांग्लादेश में हाल ही में आई बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था।
रहमान ने कहा था, ‘बांग्लादेश को अतीत का बोझ पीछे छोडक़र अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मज़बूत और संतुलित संबंध बनाए रखना चाहिए।’
शेख़ हसीना का हटना चीन के लिए मौका?
ऐसे में पाबंदी हटने के बाद जमात-ए-इस्लामी के नेताओं से चीनी राजदूत ने मुलाक़ात की।
चीनी राजदूत याओ वेन ने कहा, ‘चीन बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। चीन बांग्लादेश और बांग्लादेशियों का समर्थक है।’
शेख हसीना सरकार में बांग्लादेश का झुकाव चीन से ज़्यादा भारत की तरफ रहा।
जुलाई महीने में शेख हसीना अपना चीन दौरा बीच में छोडक़र बांग्लादेश लौट आई थीं।
इसके बाद शेख हसीना ने कहा था कि तीस्ता परियोजना में भारत और चीन दोनों की दिलचस्पी थी लेकिन वह चाहती हैं कि इस परियोजना को भारत पूरा करे।
जाहिर है कि ये बात चीन को रास नहीं आई होगी।
कहा जा रहा है कि शेख हसीना का सत्ता से बाहर होना चीन और पाकिस्तान के लिए मौके की तरह है।
चीनी राजदूत और जमात नेताओं की मुलाकात को भी इसी रूप में देखा जा रहा है।
विशेषज्ञों का क्या कहना है?
भारत के पूर्व विदेश सचिव और अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार कंवल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘चीन ने बांग्लादेश बनने का विरोध किया था। चीन ने सबसे आखऱि में बांग्लादेश को मान्यता दी।’
सिब्बल लिखते हैं, ‘जमात ने भी बांग्लादेश बनने का विरोध किया था। चीन का बांग्लादेशियों का समर्थन करने की बात खोखली है। चीन अपने देश में बांग्लादेश जैसे प्रदर्शन के बाद किसी तरह का सत्ता परिवर्तन नहीं चाहेगा। 1989 (तियानमेन स्क्वायर) को याद कर लीजिए। जमात भी चीनियों का समर्थन करता है सिवाय वीगर मुसलमानों के।’
अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने भी सोशल मीडिया पर बांग्लादेश के बदलते रुख पर टिप्पणी की है।
चेलानी लिखते हैं, ‘बांग्लादेश में सेना की बनाई अंतरिम सरकार हिंसक इस्लामिस्ट को खुली छूट दे रही है। इनके पास कोई संवैधानिक अधिकार या बहुमत नहीं है। देश के चीफ जस्टिस और पांच वरिष्ठ न्यायाधीशों को बाहर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की गई। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को वापस लेने की बात कही गई, जिसके बाद संसद ने संशोधन कर केयरटेकर सरकार के विकल्प को ख़त्म किया था। इस फ़ैसले को सुनाने वाले चीफ जस्टिस के खिलाफ हत्या का झूठा मुक़दमा दर्ज किया गया।’
लेखक तसलीमा नसरीन बांग्लादेश से हैं, मगर अपनी किताबों से हुए विवादों के कारण वो सालों से बांग्लादेश लौट नहीं सकी हैं।
2011 से तसलीमा नसरीन भारत में हैं।
द मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक- नसरीन ने कहा, ‘मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के अंतर्गत हालात और बदतर होंगे। ज़मीन पर हालात भारत विरोधी, महिला विरोधी और लोकतंत्र विरोधी है।’
पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश?
शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं रहे थे। 2018 के चुनाव में पाकिस्तानी उच्चायोग पर बांग्लादेश के चुनावों में दखल देने के आरोप भी लगे थे।
पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने नई अंतरिम सरकार के सदस्यों से मुलाकात को अहम बताया और कई क्षेत्रों में सहयोग करने की बात कही।
द जापान टाइम्स वेबसाइट पर ब्रह्मा चेलानी ने दोनों देशों को लेकर एक लेख लिखा है।
चेलानी इस लेख में लिखते हैं, ‘2022 तक बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती दिख रही थी।
लेकिन आज हालात अलग हैं। बांग्लादेश ने आईएमएफ से तीन अरब डॉलर, वल्र्ड बैंक से 1.5 अरब डॉलर और एशियन डेवलपमेंट बैंक से एक अरब डॉलर की मांग की है। विकास के मामले में पाकिस्तान की तुलना में बांग्लादेश के हालात अलग रहे।’
चेलानी ने लिखा, ‘ऐसी कई घटनाएं हैं, जिसके आधार पर सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल सकता है- जहां अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, जहां हिंसक घटनाएं होती रहती हैं। चुनावों में भी सेना की भूमिका रहती है। पाकिस्तान की ही तरह बांग्लादेश में सेना अहम भूमिका में आ गई है। सत्ता के पीछे आर्मी चीफ खड़े दिखते हैं।’
1971 युद्ध को लेकर बांग्लादेश पाकिस्तान से माफ़ी की मांग करता रहा है।
चेलानी कहते हैं- शेख हसीना की सेक्युलर सरकार में हिंसक धार्मिक समूहों पर कार्रवाई की गई। मगर अब हालात दूसरे हैं। अगर सही दिशा में कोशिशें नहीं की गईं तो बांग्लादेश पाकिस्तान का ही दूसरा रूप बन सकता है।
बांग्लादेश में जब सत्ता पलटी तो मुजीब-उर रहमान की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया।
बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता शेख़ मुजीब-उर रहमान पाकिस्तान को लेकर बहुत सख़्त रहे थे।
यहाँ तक कि शेख मुजीब-उर रहमान ने बांग्लादेश को मान्यता दिए बिना पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो (बाद में प्रधानमंत्री) से बात करने से इनकार कर दिया था।
पाकिस्तान भी शुरू में बांग्लादेश की आज़ादी को खारिज करता रहा।
बाद में पाकिस्तान के तेवर में अचानक परिवर्तन आया।
फऱवरी 1974 में ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का समिट लाहौर में आयोजित हुआ। तब भुट्टो प्रधानमंत्री थे और उन्होंने मुजीब-उर रहमान को भी औपचारिक आमंत्रण भेजा था।
पहले मुजीब ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया लेकिन बाद में इसे स्वीकार कर लिया।
इस समिट के बाद भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक त्रिकोणीय समझौता हुआ। 1971 की जंग के बाद बाकी अड़चनों को सुलझाने के लिए तीनों देशों ने नौ अप्रैल, 1974 को समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1974 में ही जुल्फिकार अली भुट्टो ने मान्यता की घोषणा करते हुए कहा था, ‘अल्लाह के लिए और इस देश के नागरिकों की ओर से हम बांग्लादेश को मान्यता देने की घोषणा करते हैं। एक प्रतिनिधिमंडल आएगा और हम सात करोड़ मुसलमानों की तरफ से उन्हें गले लगाएंगे।’
बांग्लादेश को मान्यता देने पर भुट्टो ने कहा था, ‘मैं ये नहीं कहता कि मुझे यह फैसला पसंद है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा मन खुश है। यह कोई अच्छा दिन नहीं है लेकिन हम हकीकत को नहीं बदल सकते। बड़े देशों ने बांग्लादेश को मान्यता देने की सलाह दी लेकिन हम सुपरपावर और भारत के सामने नहीं झुके। लेकिन ये अहम वक्त है। जब मुस्लिम देश बैठक कर रहे हैं, तब हम नहीं कह सकते कि दबाव में हैं। ये हमारे विरोधी नहीं हैं, जो बांग्लादेश को मान्यता देने के लिए कह रहे हैं। ये हमारे दोस्त हैं, भाई हैं।’
इस बात के करीब 50 साल हो चुके हैं और अब शेख़ हसीना के सत्ता से बाहर हो जाने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश एक दूसरे को गले लगाने की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। साथ में चीन भी खड़ा नजर आ रहा है और इस वजह से भी भारत की चिंताएं और बढ़ गई हैं। (bbc.com/hindi)
भारत में नेशनल मेडिकल कमीशन ने पाठ्यक्रम से जुड़े नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इस लेस्बियन और सोडोमी को यौन अपराध माना गया. हालांकि, क्वीयर और विकलांगता अधिकार समूहों के कड़े विरोध के बीच इसे वापस ले लिया गया है.
भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने एमबीबीएस छात्रों के लिए योग्यता-आधारित चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम (सीबीएमई) की नई गाइडलाइंस जारी की हैं। 31 अगस्त को जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों में ऐसे कुछ मुद्दों को शामिल किया गया है, जो मौजूदा दौर में एलजीबीटीक्यूए+ और महिलाओं के प्रति रूढि़वादी सोच को दर्शाते हैं। एनएमसी, मेडिकल के क्षेत्र में शिक्षा और शोध का शीर्ष नियामक है।
नई गाइडलाइंस के तहत, फॉरेंसिक मेडिसिन के पाठ्यक्रम में लेस्बियनिजम और सोडोमी को यौन अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। दिशा-निर्देश संख्या एफएम 8.4 में व्यभिचार और अप्राकृतिक यौन अपराधों के तहत इन दोनों को शामिल किया गया है। साथ ही, वर्जिनिटी और हाइमन जैसे विषय भी फिर से पाठ्यक्रम में जुड़ गए हैं।
भारत के सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत के बाहर एलजीबीटीक्यू प्लस समुदाय के दो सदस्य एक-दूसरे का हाथ पकडक़र हौसला बढ़ाते हुए। भारत के सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत के बाहर एलजीबीटीक्यू प्लस समुदाय के दो सदस्य एक-दूसरे का हाथ पकडक़र हौसला बढ़ाते हुए।
इनके अलावा, विकलांगता से जुड़ी सात घंटे की ट्रेनिंग हटा दी गई है। लैंगिक पहचान और यौन रुझान के बीच का अंतर अब मनोरोग विज्ञान के मॉड्यूल में शामिल नहीं होगा। क्वीयर लोगों के बीच सहमति से होने वाले सेक्स को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है।
लैंगिक अधिकारों के लिए तैयार नहीं एनएमसी?
सीबीएमई पाठ्यक्रम पहली बार 2019 में आयोग ने लागू किया था। करीब पांच साल बाद नए बदलावों के साथ इसे दोबारा लाया गया है। कई जानकार, संस्थाएं और अधिकार समूह पाठ्यक्रम में रूढि़वादी पक्षों को शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं। विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और ‘ट्रांसजेंडर हेल्थ इन इंडिया’ के सीईओ जॉ। संजय शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और एनएमसी को चि_ी लिखी है। इसमें नए दिशानिर्देशों को क्वीयर और विकलांगता विरोधी बताया गया है। आलोचक इन्हें ट्रांसजेंडर अधिकारों पर आए सुप्रीम कोर्ट के नालसा जजमेंट 2014 और ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऐक्ट 2019 की अवमानना भी बता रहे हैं।
समलैंगिक विवाह पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका
संजय शर्मा, ‘डॉक्टर्स विथ डिसेबिलिटीज’ नाम के संगठन से जुड़े हैं। पाठ्यक्रम में हुए ताजा बदलाव पर बात करते हुए उन्होंने डीडबल्यू हिन्दी से कहा, ये नई गाइडलाइंस हम डॉक्टरों के लिए भी एक चौंकाने वाली बात है। हम यह नहीं कह रहे कि आयोग उन बातों को शामिल करें, जो हम चाहते हैं। भारत में ट्रांसजेंडरों की सुरक्षा के लिए कानून है, विकलांग व्यक्तियों के लिए ऐक्ट है। आयोग बस उनका पालन करे, यह उसकी जिम्मेदारी भी है।
लैंगिक पहचानों पर अवैज्ञानिक और अपमानजनक रुख
संजय शर्मा ध्यान दिलाते हैं कि 2019 में जब पहली बार सीबीएमई आया, तब भी छात्रों और संबंधित पक्षों से कोई बात नहीं की गई थी। वह बताते हैं, इस मुद्दे के साथ सबसे अधिक छात्रों का हित जुड़ा हुआ है, लेकिन ना ही 2019 में उनसे बात की गई, ना ही 2024 में। ना ही इसे बनाने में क्वीयर समुदाय से किसी विशेषज्ञ को शामिल किया गया। मैं जानता हूं कि मेडकल कॉलेजों के छात्र भी इस नई गाइडलाइन के विरोध में हैं। ये मुद्दे हमारी निजी पसंद का मसला नहीं हैं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी हैं।
समलैंगिक रिश्तों को भी सुप्रीम कोर्ट ने दी परिवार की संज्ञा
इसपर डॉ. सत्येंद्र कहते हैं, उस वक्त भी आयोग ने कहा था कि ऐसी किताबों को शामिल ना किया जाए, जिसमें क्वीयर समुदाय के खिलाफ रूढि़वादी या अवैज्ञानिक बातें शामिल हैं। आयोग खुद क्यों नहीं ऐसा पाठ्यक्रम लाता है, जिसमें ये मुद्दे शामिल हों। ये नए निर्देश दिखाते हैं कि आयोग बदलावों को लेकर कितना कठोर है।
देश के कानून को नजरअंदाज करते हैं नए दिशा-निर्देश
लैंगिक पहचानों व अधिकारों से जुड़े पूर्वाग्रह और भ्रांतियां दूर करने के लिए सबसे बड़ा बदलाव तब आया था, जब 1973 में अमेरिकन साइकैट्री एसोसिएशन ने होमोसेक्शुअलिटी को मानसिक विकारों की सूची से हटाया। इसके बाद 1990 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने समलैंगिकता को मानसिक बीमारियों की अंतरराष्ट्रीय सूची से हटाया।
मेडिकल पाठ्यक्रमों और इस क्षेत्र में क्वीयर समुदाय को लेकर मौजूद पूर्वाग्रह उनके स्वास्थ्य अधिकारों के लिए एक बड़ी रुकावट हैं। इसलिए ये कदम क्वीयर और वंचित समुदायों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में सबसे जरूरी माने गए। इसके बावजूद आज भी मेडिकल क्षेत्र पूरी तरह क्वीयर और दूसरे विविध पहचानों से आने वाले लोगों के लिए पूरी तरह समावेशी नहीं बन पाया है। यह क्षेत्र आज भी महिला और पुरुष की बाइनरी पर ही आधारित है।
भारत में ट्रांसजेंडर कर रहे अलग टॉयलेट की मांग
डॉ. संजय शर्मा कहते हैं, हमारा पूरा मेडिकल सिस्टम एक बाइनरी सिस्टम है। इसमें शामिल ज्यादातर लोग भी उसी महिला-पुरुष की बाइनरी वाली सोच रखते हैं। मेडिकल पाठ्यक्रमों में जेंडर और सेक्शुअलिटी से जुड़े मुद्दे शामिल नहीं हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की जो नई गाइडलाइन आई है, उसे बनाने वाले लोगों ने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शायद इसी बाइनरी वाली सोच के दायरे में की है। बदलते वक्त के साथ उन्होंने अपनी जानकारी को अपडेट नहीं किया। इन मुद्दों पर मेडिकल साइंस कितना आगे बढ़ चुका है, कितनी ही संवेदनशील और वैज्ञानिक जानकारियां हमारे आस-पास हैं।
हाइमन का कथित महत्व पढ़ाना महिला विरोधी
आयोग ने पाठ्यक्रम में वर्जिनटी और हाइमन के कथित महत्व को भी शामिल किया है। आयोग की गाइडलाइन में ‘डिफ्लोरेशन’ शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। ये ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर पहले से ही समाज में अवैज्ञानिक और रूढि़वादी सोच गहराई तक पैठी हुई है। कुआंरेपन को लेकर चले आ रहे अस्वस्थ और विकृत विचारों ने वर्जिनिटी टेस्ट की नींव भी रखी। कुआंरेपन की जांच को डब्ल्यूएचओ मानवाधिकार हनन मानता है। भारत समेत कई देशों में इस दकियानूसी अवधारणा पर रोक लगाने के लिए अदालतों ने फैसले सुनाए हैं।
सेक्स एजुकेशन : शादी की पहली रात से जुड़े भ्रम और अंधविश्वास
डॉ.संजय शर्मा इस दृष्टिकोण से भी नए दिशा-निर्देशों को मानवाधिकार हनन मानते हैं। वह कहते हैं, अगर कोई इस जमाने में भी ऐसी गाइडलाइंस बना रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि उसे अपने देश के कानून के बारे में भी वहीं पता है। ना ही वे देश के कानून और संबंधित अधिनियमों का ध्यान रख रहे हैं, ना ही विज्ञान का। विज्ञान तो विविधिता में भरोसा करता है। ये दिशा-निर्देश राष्ट्रीय स्तर पर एक शर्म का विषय हैं।
डॉ.सत्येंद्र और डॉ. संजय, दोनों कहते हैं कि अगर एनएमसी ये दिशा-निर्देश वापस नहीं लेता, तो वे ‘वल्र्ड फेडेरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन’ को भी चिट्ठी लिखेंगे। पाठ्यक्रम में जोड़ी जा रही संबंधित चीजें फेडरेशन के मानकों के खिलाफ भी हैं।
ऐसे में अगर एनएमसी ने सुधार नहीं किया, तो वे फेडरेशन से उसकी मान्यता रद्द करने की भी मांग करेंगे। (dw.com/hi)
बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण पाकिस्तान में बाल विवाह के मामले बढ़े हैं. गरीब परिवारों में माता-पिता पैसे लेकर नाबालिग लड़कियों की शादी कर रहे हैं. 2022 की भीषण बाढ़ के बाद ऐसे मामलों में तेजी आई है.
पाकिस्तान उन देशों में है, जहां बीते सालों में जलवायु संकट के कारण बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा ज्यादा भीषण और नियमित हुई हैं। चरम मौसमी घटनाओं का एक बड़ा खामियाजा लड़कियों को उठाना पड़ रहा है। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक, मॉनसून की तेज बारिश के बाद बाढ़ के डर के कारण यहां बाल विवाह के मामले बढ़ गए हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें माता-पिता ने गरीबी की वजह से पैसे लेकर अपनी नाबालिग बेटियों की शादी कर दी।
खुशहाल जिंदगी की उम्मीद में दोगुनी उम्र के आदमी से शादी
सिंध प्रांत के दादू जिले में रहने वाली 14 साल की शमीला और उनकी 13 वर्षीय बहन अमीना के साथ यही हुआ। बाढ़ के डर के बीच बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही माता-पिता ने शमीला और अमीना की शादी कर दी। उन्होंने यह फैसला परिवार को बाढ़ के समय आने वाली किल्लत से बचाने के लिए लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि शमीला को अच्छी जिंदगी मिल सकेगी।
शमीला का पति उससे दोगुनी उम्र का है। वह कहती हैं, अपनी शादी की बात सुनकर मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा, जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। शमीला की यह उम्मीद पूरी नहीं हुई। वह बताती हैं, मेरे पास कुछ बचा नहीं। और अब दोबारा बारिश का मौसम आ रहा है तो लग रहा है कि जितना है कहीं वो भी ना चला जाए।
शमीला की सास बीबी सचल ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए शमीला के माता-पिता को दो लाख पाकिस्तानी रुपए दिए। यह बड़ी रकम है, खासकर ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जहां कई परिवार 80 रुपए के दैनिक खर्च में गुजारा करते हों।
2022 की भीषण बाढ़ का असर
यूनिसेफ के अनुसार, जलवायु संकट के कारण आ रही प्राकृतिक आपदाओं ने लड़कियों को भारी जोखिम में डाल दिया है। माशूक बरहमनी, गैर-सरकारी संगठन 'सजग संसार' के संस्थापक हैं। वह धार्मिक गुरुओं के साथ मिलकर बाल विवाह पर रोक लगाने और जागरूकता फैलाने का अभियान चलाते हैं। बरहमनी बताते हैं कि 2022 में आई भीषण बाढ़ के बाद दादू जिले के कई गांवों में बाल विवाह के मामले बढ़ गए हैं। एएएफपी से बातचीत में उन्होंने कहा, इस वजह (कुदरती आपदा) से लोग अपनी नाबालिग बच्चियों की शादियां करा रहे हैं। परिवारों को बस जिंदा रहने का साधन चाहिए होता है और इसमें पिसती हैं लड़कियां, जिनकी पैसों के बदले शादी कर दी जाती है।
साल 2022 में आई ऐतिहासिक बाढ़ में पाकिस्तान का एक तिहाई हिस्सा डूब गया। तीन करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। हजारों स्कूल, अस्पताल का नुकसान हुआ। बुनियादी ढांचे को बड़ी चोट पहुंची। दो साल बाद भी इस भीषण बाढ़ का असर महसूस किया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक, इस त्रासदी के बाद खासतौर पर वंचित वर्गों के बीच आपदाओं का डर काफी बढ़ गया है।
दक्षिण एशिया में भारत की ही तरह पाकिस्तान में भी किसानों के लिए मॉनसून की बारिश बहुत अहमियत रखती है। जुलाई से सितंबर के बीच होने यह बारिश फसल की बुआई और सिंचाई के लिए बेहद अहम है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश का मौसम लंबा और अप्रत्याशित होता जा रहा है। बेमौसम बरसात और मूसलधार बारिशें ज्यादा नियमित हो गई हैं। इसके कारण भूस्खलन और बाढ़ की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। कहीं बारिश के इंतजार में फसल सूख रही है, तो कहीं अतिवृष्टि के कारण फसल बेकार हो जाती है।
पाकिस्तान में बाल विवाह की क्या स्थिति
देश के अलग-अलग प्रांतों में शादी की न्यूनतम आयु से जुड़े नियम एक जैसे नहीं हैं। आमतौर पर यह आयुसीमा 16 से 18 साल के बीच है। जानकारों के मुताबिक, कानून को लागू करा पाना एक बड़ी चुनौती है। दिसंबर 2023 में आए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र में शादी करने वाली लड़कियों की संख्या के मामले में पाकिस्तान दुनिया में छठे स्थान पर है।
पिछले कुछ समय से बाल विवाह के मामलों में गिरावट आई थी, लेकिन अब फिर से स्थितियां खराब हो रही हैं। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से आ रही आपदाएं भी इस समस्या को बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। नियाज अहमद चांडियो, दादू में बच्चों के अधिकारों से जुड़े एक गैर-सरकारी संगठन के संयोजक हैं। उन्होंने डीडबल्यू को बताया, पिछले एक साल के दौरान दादू में बाल विवाह के 45 मामले दर्ज किए गए हैं। मेरा मानना ??है कि ऐसे और भी दर्जनों मामले हो सकते हैं, जिनका अभी तक पंजीकरण ही नहीं हुआ है। शमीला और अमीना के खान मोहम्मद मल्लाह गांव में ही पिछले मॉनसून के बाद से अब तक करीब 45 नाबालिग लड़कियों की शादी हो चुकी है।
बाल विवाह बना परिवारों के जीने का साधन
65 साल के बुजुर्ग मई हजानि भी खान मोहम्मद मल्लाह गांव के निवासी हैं। 2022 की बाढ़ के बाद हालात और मानसिकता में कैसा बदलाव आया है, इसे रेखांकित करते हुए वह बताते हैं, 2022 की भारी बरसात से पहले तक किसी को भी अपनी छोटी लड़कियों की शादी करने की जल्दी नहीं थी। लड़कियां यहां खेती करती थीं, लकड़ी के बिस्तरों के लिए रस्सियां बुनती थीं। आदमी भी मछली पकडऩे और खेती करने में व्यस्त रहते थे। कुछ ना कुछ काम हमेशा होता ही था।
लोगों का कहना है कि अब उन्हें बेटियों को ब्याहने की जल्दी है। कई ग्रामीणों ने एएफपी को बताया कि आमतौर पर वे पैसे लेकर बेटियों की शादी कर देते हैं। इससे परिवार की भी आमदनी होती है और उन्हें लगता है, बेटियां भी गरीबी से निकल जाएंगी। ऐसे भी मामले सामने आएं हैं, जहां लड़क़े के परिवार ने शादी की रकम देने के लिए कर्ज लिया और फिर कर्ज चुकाने में नाकाम रहने पर लडक़ा पत्नी समेत अपनी ससुराल में रहने लगा।
नजमा अली और उनके पति की आपबीती ऐसी ही है। 2022 की बाढ़ के बाद माता-पिता ने महज 14 साल की उम्र में नजमा की शादी कर दी। शादी के समय नजमा काफी खुश थीं। वह बताती हैं, मेरे पति ने मेरे माता-पिता को ढाई लाख रुपए दिए, वो भी कर्ज लेकर। अब वह कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। अपने छह महीने के बच्चे का पालना झुलाते हुए नजमा आगे कहती हैं, मैंने सोचा था कि मैं नए कपड़े लूंगी, लिपस्टिक लाऊंगी, नए बर्तन खरीदूंगी। लेकिन अब मैं वापस अपने माता-पिता के पास आ गई हूं, पति और बच्चे को लेकर।
जलवायु संकट के कारण रोजी-रोटी के लाले
नजमा, नैरा घाटी के एक गांव में रहती हैं। यह भी सिंध प्रांत का इलाका है। यहां पानी इतना प्रदूषित है कि सारी मछलियां मर चुकी हैं। नजमा की मां कहती हैं, हमारे धान के खेत हुआ करते थे, जहां हमारी बेटियां भी काम करती थीं। वहां हम सब्जियां भी उगाते थे। अब पानी इतना जहरीला हो गया कि वहां सब कुछ खत्म हो चुका है। यह खासकर 2022 के बाद हुआ है। नजमा की मां कहती हैं, पहले लड़कियां बोझ नहीं हुआ करती थीं, लेकिन अब ऐसा है कि जिस उम्र में लड़कियों की कायदे से शादी होनी चाहिए, उस उम्र में उनके 3-4 बच्चे हैं। और फिर वो वापस भी आ जाती हैं अपने माता-पिता के साथ रहने क्योंकि उनके पति काम नहीं करते।
2022 की बाढ़ का साफ पानी की आपूर्ति और जल स्रोतों पर बड़ा असर पड़ा। बड़ी संख्या में तालाब और कुएं प्रदूषित हो गए। उनका पानी पीने लायक नहीं बचा। 2023 में आई यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बाढ़ प्रभावित इलाकों में करीब 54 लाख लोग अब भी अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह प्रदूषित पानी पर निर्भर हैं।
बाल विवाह के नुकसानों पर जागरूकता की जरूरत
मौसमी संकट तो है ही, लेकिन पाकिस्तान के पितृसत्तात्मक समाज ने भी इस संकट को बड़ा बनाने में अहम भूमिका निभाई है। पर्यावरण और लैंगिक मुद्दों पर काम कर रहीं पत्रकार आफिया सलाम ने डीडब्ल्यू को बताया, यहां लड़कियों को बोझ समझा जाता है। जल्द-से-जल्द उनकी शादी करने की कोशिश की जाती है। वह मानती हैं कि इस मुद्दे पर व्यापक जागरूकता की जरूरत है।
बाल विवाह के कारण लड़कियां जल्दी मां भी बन जाती हैं और आगे चलकर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं। शिक्षा और रोजगार की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं, जिससे वे असुरक्षित महसूस करती हैं और पूरी तरह से अपने परिवारों पर निर्भर रहती हैं। ऐसे में सरकार, प्रशासन और सिविल सोसायटी की और से ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। समय रहते दखल दिया जाए तो कुछ बदलाव हासिल हो सकते हैं, जैसा कि महताब के साथ हुआ। महताब का परिवार भी 2022 की बाढ़ से प्रभावित हुआ। वे राहत शिविर में ही थे, जब उनके पिता दिलदार अली शेख ने महताब की शादी तय कर दी। उस समय महताब मात्र 10 साल की थीं।
गैर-सरकारी संगठन सुजग संसार के हस्तक्षेप के कारण महताब की ना केवल शादी टल गई, बल्कि संगठन ने एक सिलाई की वर्कशॉप में भी उनका दाखिला कराया। इसके कारण महताब की पढ़ाई भी जारी रही और वह थोड़ा-बहुत कमाने भी लगीं। लेकिन जब मॉनसून आता है, महताब को शादी का डर सताने लगता है। वह कहती हैं, मैंने अपने पिता से कहा है कि मैं पढऩा चाहती हूं। मैं अपने आस-पास शादीशुदा लड़कियां देखती हूं जिनकी जिंदगी बहुत मुश्किल है। मैं अपने लिए ऐसा नहीं चाहती।एसके/एसएम (एएफपी)
-कीर्ति दुबे
जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से केसी त्यागी का इस्तीफा नीतीश कुमार की पार्टी की उलझन की ओर इशारा करता है।
केसी त्यागी जिस जेडीयू के प्रवक्ता थे, वह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। जेडीयू केंद्र सरकार में भी शामिल है और बिहार में भी बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रही है।
लेकिन केसी त्यागी जेडीयू की बात जिस तरह से मीडिया के सामने रख रहे थे, उससे कई बार लगता था कि वह उस जेडीयू के प्रवक्ता हैं, जब नीतीश कुमार का तेवर 2017 से पहले वाला हुआ करता था।
केसी त्यागी की टिप्पणी से एनडीए की लाइन के बचाव से ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे थे। उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों पर जमकर सवालिया निशान लगाए थे। खासकर लैटरल एंट्री, इसराइल, गाजा और अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी के मामले में।
बीते रविवार को जेडीयू ने केसी त्यागी की जगह राजीव रंजन को पार्टी का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया।
इससे पहले मार्च 2023 में केसी त्यागी ने प्रवक्ता के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था लेकिन दो महीने बाद ही उनकी वापसी हो गई थी। अब दो साल में दूसरी बार उन्होंने ये पद छोड़ा है।
अपने इस्तीफे पर केसी त्यागी की सफाई
बीबीसी से खास बातचीत में केसी त्यागी ने अपने इस्तीफे, राहुल गांधी, जेडीयू की आंतरिक राजनीति और प्रशांत किशोर की विधानसभा चुनाव में एंट्री जैसे कई मुद्दों पर बात की।
अपने इस्तीफ़े पर उन्होंने कहा, ‘नीतीश कुमार अब जब अध्यक्ष नहीं रहे तो लगा मुझे ये पद छोड़ देना चाहिए। पिछले दो-ढाई सालों से मैं संगठन के पद पर नहीं हूँ। बस पार्टी का प्रवक्ता था और मुख्य सलाहकार हूँ। पिछले कुछ समय से मैं लेखन के काम में लगा हुआ हूं। लिहाजा मैंने नीतीश कुमार से आग्रह किया कि मुझे पार्टी के पदों से मुक्त किया जाए। मेरा नीतीश कुमार से 48 सालों का रिश्ता है। वो मेरे नेता भी हैं और मित्र भी।’
केसी त्यागी कहते हैं, ‘मैं एक बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि मैं इस पार्टी में नीतीश कुमार की वजह से हूँ। जहाँ तक अखबारों में चर्चा है, मेरा कोई भी बयान ऐसा नहीं है, जो जेडीयू की विचारधारा से मेल ना खाता हो और एक भी बयान बीजेपी के खिालफ नहीं है।’ महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में जातिगत जनगणना कराई। इसके बाद वो फिर बीजेपी के साथ हो लिए।
बीते दिनों आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा था, ‘जातिगत जनगणना संवदेनशील मामला है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक या चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसका इस्तेमाल पिछड़े समुदाय और जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए।’
ये बयान बीजेपी के जातिगत जनगणना पर दिए गए पिछले बयानों से अलग है।बीते साल छत्तीसगढ़ की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, ‘गरीब ही सबसे बड़ी जाति और सबसे बड़ी आबादी है। कांग्रेस देश में हिन्दुओं को बाँट रही है।’
केसी त्यागी संघ के बयान को बीजेपी की ओर से जातिगत जनगणना के प्रति सकारात्मक पहल के रूप में देखते हैं।
क्या नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए हैं?
नीतीश कुमार मोदी 3.0 सरकार के लिए कई बार ये दोहराते दिखते हैं कि इस सरकार को जेडीयू का ‘बेशर्त समर्थन’ है।
अगर संख्या बल देखें तो इस एनडीए सरकार में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दो ऐसे नेता हैं जो सरकार को बरकरार रखने और गिराने का दम रखते हैं।
ऐसे में जेडीयू का इतना अहम समर्थन होने के बाद भी नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं ले पा रहे?
केसी त्यागी इस पर कहते हैं, ‘बजट में बिहार के लिए हजारों करोड़ दिए गए हैं। बिहार में मेडिकल कॉलेज बनेंगे, हवाईअड्डे बनेंगे, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। विशेष राज्य बनाने की दिशा में केंद्र सरकार का बड़ा कदम है।’
बतौर जेडीयू नेता केसी त्यागी भले ये कह रहे हों लेकिन बिहार की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग इसे नीतीश कुमार का मोदी सरकार के सामने झुके हुए बर्ताव की तरह देखते हैं।
पटना में एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज के पूर्व निदेशक डीएम दिवाकर कहते हैं, ‘केंद्र में एनडीए सरकार के लिए उनका समर्थन काफी अहम है। नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में हैं कि वो चाहें तो कई मांगें बिहार को लेकर मनवा सकते हैं, लेकिन वो हर जगह यही कहते हैं कि हमारा बीजेपी को समर्थन बिना शर्त के है। आज एनडीए सरकार में जो हैसियत जेडीयू की है, इसके बावजूद नीतीश कुमार का दंडवत होने वाला रवैया मुझे समझ नहीं आता।’
केसी त्यागी समाजवादी आंदोलन से जुड़े नेता हैं। जेडीयू की कमान चाहे शरद यादव के हाथ में रही हो या ललन सिंह के पास, केसी त्यागी हमेशा ही नीतीश कुमार के कऱीबी रहे।
केसी त्यागी ने 1974 में चौधरी चरण सिंह के साथ काम किया और साल 1989 में लोकसभा सांसद रहे।
इससे पहले त्यागी जॉर्ज फर्नांडीस के साथ इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन में रहे और यहीं से समाजवाद की राजनीति में उनका कद बढ़ा।
खेमा बदलने पर नीतीश का बचाव
क्या केसी त्यागी के लिए बार-बार नीतीश कुमार के खेमा बदलने का बचाव करना और जायज ठहराना मुश्किल रहा है?
इस सवाल पर वो कहते हैं, ‘नहीं। नीतीश कुमार ने बिहार के भले के लिए किया और मुझे इसका बचाव करने में कोई संकोच नहीं हुआ।’
लेकिन जो लोग केसी त्यागी को करीब से जानते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि त्यागी समाजवादी नेता हैं और विचारधारा के बिल्कुल उलट कुछ बोल पाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था।
बिहार की राजनीति में जाना-माना नाम शिवानंद तिवारी जेडीयू में भी रहे और अब आरजेडी में हैं। समाजवाद के आंदोलन से निकले शिवानंद तिवारी केसी त्यागी को काफी करीब से जानते हैं।
शिवानंद तिवारी केसी त्यागी को लेकर कहते हैं, ‘केसी त्यागी को हम 1977 के वक्त से जानते हैं। वो समाजवादी हैं। अपनी विचारधारा पूरी तरह नहीं बदल देंगे। गाजा में जो हो रहा है, उनकी राय वही रहेगी जो हमारी राय है। लेकिन आज के समय में वैचारिक प्रतिबद्धता आसान नहीं है।’
शिवानंद तिवारी कहते हैं, ‘आजकल नेता बॉस के अंदाज में काम करते हैं। मैं जेडीयू में रहा और आरजेडी में भी। मुझे नहीं पता कि केसी त्यागी जी ने इस्तीफा क्यों दिया है लेकिन जो मैं अखबारों में ही पढ़ रहा हूं उससे तो यही लगता है कि उनके बयान बीजेपी को और जेडीयू के नेतृत्व को असहज कर रहे थे।’
विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता और वोट बैंक की राजनीति
एक वक्त था, जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को बिहार में चुनाव प्रचार तक करने नहीं आने देते थे।
साल 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया था। इसे नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्षता को लेकर प्रतिबद्धता के रूप में देखा जाता था। अब चीज़ें पूरी तरह से बदल गईं। नीतीश कुमार को बीजेपी अपने हिसाब से कई बार झुका चुकी है।वर्तमान समय में नीतीश कुमार मोदी सरकार को बिना शर्त समर्थन की बात करते हैं। भारत की राजनीति में अब अक्सर कहा जाता है कि धर्मनिरेपक्षता वैचारिक प्रतिबद्धता से ज्यादा वोट बैंक सुनिश्चित करने का जरिया है। नीतीश कुमार के पाला बदलने को इसी से जोड़ा जाता है।
केसी त्यागी नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहते हैं, ‘जब जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हुआ तो हमारी पार्टी ने वॉकआउट किया था। यूसीसी पर भी नीतीश कुमार ने कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं लेकिन इसके स्टेकहोल्डर्स से बात की जानी चाहिए।’
वो कहते हैं, ‘जब मैंने एनडीए उम्मीदवार के रूप में मेरठ से चुनाव लड़ा तो मुस्लिम वोट बीएसपी को पड़े लेकिन इससे मेरी वैचारिक प्रतिबद्धता थोड़ी भी नहीं डगमगाई। मैं या नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष हैं और ये प्रतिबद्धता वोटबैंक के लिए नहीं है।’ हाल के वर्षों में धर्म के आधार पर लिंचिंग की कई घटनाएं हुई हैं।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा अक्सर एक समुदाय को टारगेट करने वाला बयान देते हैं। हाल ही में उनकी सरकार ने असम में विधानसभा सत्र के दौरान जुमे की नमाज के लिए मिलने वाला वक्त खत्म कर दिया था।
असम सरकार के इस फैसले पर केसी त्यागी कहते हैं, ‘हम इस फैसले के पूरी तरह खिलाफ हैं और ये नहीं होना चाहिए।’
बिहार चुनाव और प्रशांत किशोर की एंट्री
बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं और इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर ने एंट्री ली है। लगभग दो साल से वो बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। उनकी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में उनकी पार्टी क्या कोई अहम भूमिका निभा सकती है?
इस सवाल पर त्यागी कहते हैं, ‘बिहार का चुनाव दोतरफा है। एक तरफ है, बीजेपी और जेडीयू तो दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन होगा। ये चुनाव भी गठबंधन में बँटा होगा। यहां की राजनीति में किसी भी तीसरे दल की जगह नहीं है। प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा उन्हें बिहार चुनाव में कुछ हासिल नहीं होगा। वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे।’
साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ थे। तब प्रशांत किशोर ने नारा दिया था- बिहार में बहार है, नीतीशे कुमार है।
दोनों के बीच घनिष्ठता ऐसी बढ़ी थी कि नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया लेकिन ये साथ लंबा नहीं चला और प्रशांत किशोर ने जेडीयू छोड़ दी।
लेकिन नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच वास्तव में हुआ क्या था?
इस पर केसी त्यागी कहते हैं, ‘नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को पार्टी का सोल वाइस प्रेजिडेंट बनाया, जिसका मतलब है कि उनकी जानकारी के बिना पार्टी में कोई फैसला नहीं हो सकता था। लेकिन वही बताएंगे कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी। जेडीयू में रहते हुए उन्होंने ममता बनर्जी का कैंपेन संभाला, तमिलनाडु में डीएमके लिए काम किया। हम और नीतीश कुमार 40 साल से साथ हैं और हमने तो आज तक दल नहीं बदला, दल के प्रति निष्ठा अलग चीज़ है।’
इंडिया गठबंधन बनाने का आइडिया नीतीश कुमार का था। उन्होंने पटना में इसकी बैठक कराई। लेकिन फिर उन्होंने ख़ुद को इस गठबंधन से अलग किया और फिर से बीजेपी के साथ चले गए।
नीतीश कुमार के इंडिया ब्लॉक छोडऩे की वजह बताते हुए केसी त्यागी कहते हैं, ‘इंडिया ब्लॉक में ये तय हुआ था कि प्रधानमंत्री के लिए कोई नाम तय नहीं होगा। फिर ममता बनर्जी ने एक बैठक में कहा कि मल्लिकार्जुन खडग़े जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया जाए। जब ये तय हुआ था कि कोई उम्मीदवार उम्मीदवार नहीं होगा तो ऐसा क्यों हुआ?’
केसी त्यागी कहते हैं, ‘उस पर भी सबके सामने बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश जी ममता जी के प्रस्ताव पर राजी नहीं हैं। इसके बाद ही नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक छोडऩे का मन बना लिया। राहुल गांधी ये बात नीतीश जी से अकेले में भी कर सकते थे लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा वो ही हमारे गठबंधन छोडऩे का कारण बना।’ (bbc.com/hindi)
-अपूर्व
कभी अमरनाथ से कटरा जा रही बस के ड्राइवर सलीम शेख गुजरात के तीर्थ यात्रियों को आतंकी हमले से बचाते हैं, तो कभी आशिक अली गंगा में डूबने से कावडिय़े को बचाते हैं। कोरोना के दौरान मुंबई में मुस्लिम बहुल बस्ती में हिन्दू बुजुर्ग की मौत होने के बाद पड़ोसी मुस्लिमों ने पूरे हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करवाया।
दरअसल, ये खबरें आम हैं। रोज की बात है पर आज का मीडिया इन्हें तवज्जो नहीं देता क्योंकि इसमें प्यार है।
आपको याद है शैल देवी मुजफ्फरपुर की जिन्होंने कई मुस्लिम परिवार की जान बचाई थी और तत्कालीन सीएम मांझी ने उन्हें झाँसी की रानी कह कर प्रशंसा की, पुरस्कृत किया था।
उत्तराखंड के डोईवाला(देहरादून) के हिंदू और मुस्लिम परिवार ने हिमालयन अस्पताल में भर्ती एक-दूसरे के बेटे को किडनी देते हैं।
ऐसी खबरें ही नहीं इससे ज़्यादा प्यार है पर जिस मीडिया को आप देखते पढ़ते हैं उसके लिए ये खबरें नहीं?
वैसे ठीक भी है जो प्यार-दोस्ती हमेशा रही हो और हर समय कायम हो वो खबर क्यों बने?
इतिहास के पन्ने पलटिये ये प्यार हर पन्ने में दर्ज है ।
प्रेमचंद जब अपने अंतिम दिनों में तबियत खराब होने के चलते लखनऊ इलाज के लिए पहुंचे तो कुछ दिन अपने दोस्त कृपा शंकर निगम के घर रुके। इसके बाद अमीनाबाद के सूर्य होटल चले गए।
यहाँ पता चला उन्हें ‘लिवर सिरोसिस’ है।
काफी गंभीर हो गए थे प्रेमचंदजी, उन्हें इलाज के साथ देखरेख की भी उतनी ही जरूरत थी ।
लखनऊ में ही प्रेमचंद के एक दोस्त थे, आर्टिस्ट अब्दुल हकीम साहब। उनका घर बहुत छोटा था पर दिल बड़ा वो मुंशी प्रेमचंद जी को होटल से जबरदस्ती आग्रहपूर्वक, अधिकार से अपने घर ले आये।
प्रेमचंद के सुपुत्र अमृत राय ने लिखा है कि ‘...अब्दुल हकीम साहब ने बिल्कुल अपने सगे भाई की तरह उनकी सेवा की, कमोड तक साफ किया, धुन्नू [बड़े बेटे] को सुला देते और खुद रात-रात भर जागते मगर चेहरे पर शिकन नहीं।
अब्दुल हकीम साहब और प्रेमचंद जी का प्यार इस मिट्टी में शामिल है, ये हमेशा महकता रहेगा और ये मोहब्बत बनी रहेगी।
-रेहान फजल
लैटरल एंट्री को लेकर पिछले दिनों काफी विवाद रहा और मोदी सरकार ने 45 पदों पर होने वाली नियुक्ति रोक दी। लेकिन मोदी सरकार 2018 से अब तक बड़ी तादाद में पेशेवर लोगों को लैटरल एंट्री दे चुकी है और उसके पहले भी यह सिलसिला लगातार जारी रहा है।
दरअसल, इसकी शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने ही कर दी थी।
जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और उनकी टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि किस तरह नए देश का बुनियादी ढाँचा खड़ा किया जाए।
नए देश के सामने युद्ध, सूखे और सांप्रदायिक तनाव की समस्या मुँह बाए खड़ी थी।
आईसीएस (अँग्रेजों के जमाने के इंडियन सिविल सर्विसेज) के लिए आखिरी परीक्षा सन् 1943 में हुई थी और आजादी के बाद कई आईसीएस अफसरों ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया था।
एक पत्रकार को मिली विदेश सेवा में लैटरल एंट्री
खाली प्रशासनिक पदों को भरने के लिए तुरंत कोई परीक्षा कराई नहीं जा सकती थी इसलिए नेहरू सरकार ने इन पदों पर बिना परीक्षा के लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया था।
इनमें से कई लोग सेना, ऑल इंडिया रेडियो और वकालत के पेशे से चुने गए थे। सबसे पहले भारतीय विदेश सेवा के लिए चुने गए लोगों में पीआरएस मणि का नाम आता है।
उन्होंने सन् 1939 में ऑल इंडिया रेडियो मद्रास में पब्लिसिटी असिस्टेंट और उद्घोषक के तौर पर अपना करियर शुरू किया था।
अपने रेडियो के करियर के दौरान वो जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आए और जब 1946 में नेहरू ने मलाया का दौरा किया तो वो ‘फ्री प्रेस जर्नल’ के रिपोर्टर के तौर पर उनके साथ वहाँ गए।
मणि की पहली पोस्टिंग इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारतीय दूतावास में प्रेस अताशे के तौर पर की गई थी।
कल्लोल भट्टाचार्जी अपनी किताब नेहरूज फस्र्ट रेक्रूट्स में लिखते हैं, मणि के प्रयासों का ही नतीजा था कि भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे थे। ये काम विदेश सेवा के किसी अधिकारी की बदौलत नहीं बल्कि पीआरएस मणि के उत्साही प्रयासों की बदौलत हुआ था।
सन् 1995 में इंडोनेशिया की सरकार ने पीआरएस मणि को अपने सबसे बड़े राजकीय पुरस्कार फस्र्ट क्लास स्टार ऑफ सर्विस से सम्मानित किया था। मणि के बाद ऑल इंडिया रेडियो में अंग्रेजी का समाचार पढऩे वाले रणबीर सिंह को भारतीय विदेश सेवा में सीधे नियुक्त किया गया था। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो के ही एआर सेठी को भारतीय विदेश सेवा में लिया गया था।
लैटरल एंट्री से नियुक्तियां
परमेश्वर नारायण हक्सर इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत किया करते थे। वो कांग्रेस के नेता और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी के दोस्त हुआ करते थे।
उन्हें भी अक्तूबर, 1947 में नेहरू ने विदेश मंत्रालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया था। इसके बाद वो नाइजीरिया और ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत रहे। दो दशक बाद जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं तो उन्होंने उन्हें अपना प्रधान सचिव नियुक्त किया था।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डिग्री लेने के बाद वो 30 के दशक में इंग्लैंड गए थे, जहाँ उन्होंने मशहूर एंथ्रोपॉलॉजिस्ट ब्रोनिसलॉ मेलिनोस्की की देखरेख में मानवशास्त्र की पढ़ाई की थी।
जयराम रमेश हक्सर की जीवनी ‘इंटरट्वाइंड लाइव्स पीएन हक्सर एंड इंदिरा गांधी’ में लिखते हैं, हक्सर के बारे में कहा जाता था कि आधुनिक भारत के नाजुक मोड़ पर वो न सिर्फ यहाँ के सबसे ताक़तवर नौकरशाह थे, बल्कि इंदिरा गांधी के बाद भारत के दूसरे सबसे ताकतवर इंसान भी थे और उनकी ताकत का स्रोत इंदिरा गांधी नहीं थीं।
चीफ ऑफ प्रोटोकॉल मिर्जा राशिद बेग
विदेश मंत्रालय में सीधे प्रवेश पाने वाले एक और शख्स थे मिर्जा राशिद अली बेग। बेग ने सेना के अफसर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वो मोहम्मद अली जिन्ना के निजी सचिव बन गए थे।
पाकिस्तान की स्थापना के मुद्दे पर उनसे मतभेद होने पर उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था।
सन् 1952 में उन्हें फि़लीपींस में तैनात किया गया था। वो बाद में भारत के सबसे सफल चीफ ऑफ प्रोटोकॉल बने।
अपने चर्चित कार्यकाल के दौरान उन्होंने दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर, सोवियत प्रधानमंत्री ख्रूश्चेव, चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, वियतनामी नेता हो ची मिन्ह, ब्रिटेन की महारानी एलेजाबेथ, मिस्र के राष्ट्रपति जमाल नासेर, सऊदी अरब के शाह सऊद, ईरान के शाह और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव डैग हैमरशोल्ड जैसे नेताओं का स्वागत किया।
खुशवंत सिंह की भी हुई लैटरल एंट्री
आजादी के बाद खान अब्दुल गफ्फार खान के भांजे मोहम्मद यूनुस को भी नेहरू ने विदेश मंत्रालय में नियुक्त किया। यूनुस तुर्की, इंडोनेशिया और स्पेन में भारत के राजदूत रहे और 1974 में वाणिज्य सचिव होकर रिटायर हुए।
बाद में उन्हें ट्रेड फेयर अथॉरिटी का प्रमुख बनाया गया। वो अंत तक इंदिरा गाँधी के करीब रहे। 1977 में जब इंदिरा गांधी चुनाव हारीं और सांसद नहीं रह गईं तो उन्होंने उन्हें 12 विलिंग्टन क्रेसेंट का अपना घर रहने के लिए दे दिया था।
विदेश मंत्रालय में सीधी नियुक्ति पाने वालों में मशहूर कवि हरिवंशराय बच्चन भी थे। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के लेक्चरर थे।
कैंब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की थी। वहाँ से लौटने पर वो आकाशवाणी इलाहाबाद में प्रोड्यूसर के तौर पर नियुक्त हो गए थे।
जवाहरलाल नेहरू की पहल पर उन्हें विदेश मंत्रालय मे हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के तौर पर नियुक्त किया गया था।
कल्लोल भट्टाचार्जी लिखते हैं, बच्चन की सलाह पर ही बाहरी मामलों के मंत्रालय का नाम विदेश मंत्रालय रखा गया था।
उन्होंने गृह मंत्रालय का नाम देश मंत्रालय सुझाया था लेकिन इसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया था।
उन्होंने विदेश मंत्रालय में आने वाले कई अफसरों को हिंदी पढ़ाई थी। बाद में विदेश मंत्री बने नटवर सिंह उनमें से एक थे।
मशहूर लेखक खुशवंत सिंह को भी लैटरल एंट्री मिली थी। उस समय वो लाहौर में वकालत कर रहे थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप सचिव अजीम हुसैन के कहने पर उन्हें लंदन में भारतीय उच्चायोग में सूचना अधिकारी की नौकरी मिली थी। बाद में इसी पद पर उनका तबादला कनाडा की राजधानी ओटावा में कर दिया गया था। वहाँ उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
इसके बाद वो पत्रकारिता में चले गए थे और योजना, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और नेशनल हेरल्ड के संपादक के तौर पर उन्होंने काफी नाम कमाया था।
केआर नारायणन की नियुक्ति
सरोजिनी नायडू की बेटी लीलामणि नायडू ने भी विदेश मंत्रालय में सीधे प्रवेश किया था। सन् 1941 से 1947 तक वो ओस्मानिया विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग की प्रमुख थीं।
इसके बाद वो हैदराबाद के निजाम कॉलेज में दर्शन शास्त्र विभाग की प्रमुख हो गईं थीं। वहाँ से उन्हें सीधे विदेश मंत्रालय में सीनियर स्केल में नियुक्त किया गया था।
सन् 1948 में पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में उन्हें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का सलाहकार नियुक्त किया गया था।
नेहरू की सिफारिश पर विदेश मंत्रालय में नौकरी पाने वालों में केआर नारायणन भी थे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने।
वो लंदन स्कूल ऑफ़ इकॉनॉमिक्स के प्रोफेसर लास्की का नेहरू के नाम एक पत्र लेकर आए थे जिसमें लास्की ने उनकी बहुत तारीफ की थी।
सन् 1949 में उनकी पहली पोस्टिंग सेकेंड सेक्रेट्री के रूप में बर्मा में की गई थी।
सन् 1950 से 1958 के बीच उन्होंने टोक्यो और लंदन के भारतीय दूतावासों में काम किया था। सन 1976 में उन्हें चीन में भारत का राजदूत बनाया गया था।
इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुल की स्थापना
सन 1959 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उच्च पदों को भरने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने औद्योगिक प्रबंधन पुल (इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पूल) की स्थापना की थी।
इसमें पूरे भारत से कुल 131 पेशेवर लोगों को चुना गया था। इनमें से कई लोग जैसे मंतोष सोंधी, वी कृष्णामूर्ति, मोहम्मद फजल और डीवी कपूर जैसे लोग सचिव स्तर तक पहुंचे थे।
इससे पहले सन् 1954 में अर्थशास्त्री आईजी पटेल को पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आर्थिक उप-सलाहकार नियुक्त किया गया था। बाद में वो आर्थिक मामलों के सचिव और रिजर्व बैंक के गवर्नर भी बने थे।
सन् 1971 में मनमोहन सिंह को वाणिज्य मंत्रालय में सलाहकार के तौर पर लाया गया था। इससे पहले वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे।
मनमोहन सिंह आर्थिक मामलों के सचिव, रिज़र्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद संभालने के बाद भारत के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे।
जारी रहा सिलसिला
जनता सरकार के जमाने में रेलवे इंजीनयर एम मेंज़ेस को सीधे रक्षा उत्पादन मंत्रालय का सचिव बनाया गया था।
राजीव गांधी ने केरल इलेक्ट्रॉनिक डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रमुख केपीपी नाम्बियार को इलेक्ट्रॉनिक्स सचिव नियुक्त किया था।
उसी जमाने में सैम पित्रोदा को सीधे अमेरिका से लाकर सेंटर फॉर डेवेलपमेंट ऑफ़ टेलीमेटिक्स (सी-डॉट) का प्रमुख बनाया गया था।
1980 और 90 के दशक में कई टेक्नोक्रैटेस जैसे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, राकेश मोहन, विजय केलकर और बिमल जालान जैसे लोगों को अतिरिक्त सचिव के स्तर पर नौकरशाही में शामिल किया गया था जो बाद में सचिव स्तर तक पहुंचे थे।
अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में आरवी शाही को निजी क्षेत्र से लाकर सीधे पावर सेक्रेट्री बनाया गया था।
मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भी नंदन नीलेकणि को निजी कंपनी इन्फोसिस से लाकर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का प्रमुख बनाया गया था।
सन् 2018 से अब तक 63 लोगों को संयुक्त सचिव स्तर पर नौकरशाही में शामिल किया गया है, जिनमें से 35 अधिकारी निजी क्षेत्र से लिए गए हैं। (bbc.com/hindi)
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण देना भारत के लिए एक कूटनीतिक संकट बन सकता है. बांग्लादेश के लोग हसीना की वापसी चाहते हैं, लेकिन भारत के लिए उन्हें भेजना आसान नहीं होगा.
बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़े एक महीने से ज्यादा हो गया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने भारत में शरण ली थी। विशेषज्ञों का कहना है कि उन्हें शरण देना अब भारत के लिए कूटनीतिक सिरदर्द बनता जा रहा है।
शेख हसीना का सख्त शासन पिछले महीने उस समय समाप्त हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने ढाका में उनके महल की ओर मार्च किया। 15 साल के उनके शासनकाल के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन और विपक्ष पर दमन के कई आरोप लगे थे।
उनकी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्र अब हसीना की वापसी की मांग कर रहे हैं ताकि उन पर विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों की हत्या के लिए मुकदमा चलाया जा सके। भारत हसीना के शासनकाल के दौरान उनका सबसे बड़ा समर्थक था। अब उन्हें वापस भेजना भारत के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि इससे दक्षिण एशिया में उसके अन्य पड़ोसियों के साथ संबंध खराब होने का जोखिम है, जहां चीन के साथ प्रभाव के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है।
मुश्किल है शेख हसीना की वापसी
इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के थॉमस कीन ने कहा, भारत स्पष्ट रूप से उन्हें बांग्लादेश वापस भेजना नहीं चाहेगा। जो अन्य नेता दिल्ली के करीबी हैं, उनके लिए यह संदेश बहुत सकारात्मक नहीं होगा कि आखिरकार, भारत आपकी रक्षा नहीं करेगा।
पिछले साल मालदीव में भारत के पसंदीदा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की हार से भारत को पहले ही एक बड़ा झटका लग चुका है। वहीं शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने से भारत का क्षेत्र में निकटतम सहयोगी भी छिन चुका है।
हसीना के शासन में पीडि़त लोगों में भारत के प्रति खुलेआम गुस्सा है। यह गुस्सा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू-राष्ट्रवादी सरकार की नीतियों और बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के खिलाफ जोर-शोर से चलाए गए प्रचार के कारण और भी गहरा हो गया है।
मोदी ने 84 वर्षीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस द्वारा गठित नई सरकार को समर्थन देने का वादा किया है, जो हसीना के बाद सत्ता में आई है। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के हिंदू धार्मिक अल्पसंख्यक की सुरक्षा की भी जोरदार मांग की है।
हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले
बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में गृह विभाग के सलाहकार जनरल एम शखावत हुसैन ने माना है कि अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं और उनकी सुरक्षा में चूक हुई है। उन्होंने हिंदुओं से इसके लिए माफी भी मांगी। हिंदू परिवारों का कहना है कि इस हिंसा ने 1971 के मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना की ओर से किए गए अत्याचार के जख्मों को ताजा कर दिया है। कुछ इलाकों से हिंदुओं के मोहल्लों और मंदिरों की सुरक्षा में तैनात मुस्लिम युवकों की तस्वीरें और खबरें भी सामने आईं लेकिन इनके मुकाबले हमले की घटनाएं कहीं ज्यादा थीं। ऐसी खबरें हैं कि सांप्रदायिक तनाव और बढ़ सकता है।
हसीना की अवामी लीग को बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अधिक समर्थक माना जाता था, जबकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में बांग्लादेशी हिंदुओं के खतरे में होने की बात कही और बाद में इस मुद्दे को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी उठाया।
हसीना के देश छोडऩे के बाद हुए हमलों में कुछ बांग्लादेशी हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाया गया था, जिसकी निंदा छात्र नेताओं और अंतरिम सरकार ने की। लेकिन भारतीय समाचार चैनलों ने इस हिंसा को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, जिससे हिंदू संगठनों ने मोदी की पार्टी से जुड़े हुए विरोध प्रदर्शन किए।
भारत की कूटनीतिक उलझन
बीएनपी के एक शीर्ष नेता फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा, भारत ने सभी अंडे एक ही टोकरी में रख दिए हैं और अब वह अपनी नीति को बदलने का रास्ता नहीं खोज पा रहा है। उन्होंने एएफपी से कहा, बांग्लादेश के लोग भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन अपने हितों की कीमत पर नहीं।
बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी दोनों देशों के बीच अविश्वास की भावना स्पष्ट है। अगस्त में बाढ़ के दौरान जब दोनों देशों में मौतें हुईं, तो कुछ बांग्लादेशियों ने इसके लिए भारत को दोषी ठहराया।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सार्वजनिक रूप से भारत में शरण लिए हसीना के मुद्दे को नहीं उठाया है, लेकिन ढाका ने उनका कूटनीतिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है, जिससे वह आगे यात्रा नहीं कर सकेंगी। दोनों देशों के बीच 2013 में हस्ताक्षरित एक प्रत्यर्पण संधि है जो हसीना को आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए वापस भेजने की अनुमति देती है। हालांकि, संधि में एक प्रावधान है जो कहता है कि यदि अपराध राजनीतिक स्वभाव का हो, तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है।
भारत के पूर्व राजदूत पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने कहा कि द्विपक्षीय संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं और ढाका इसे बिगाडऩे के लिए हसीना के मुद्दे को तूल नहीं देगा। उन्होंने एएफपी से कहा, कोई भी परिपक्व सरकार समझेगी कि हसीना के भारत में रहने को मुद्दा बनाना उनके लिए कोई लाभ नहीं देगा। (डॉयचेवैले)
डॉनल्ड ट्रंप ने जेडी वैंस को अपने उपराष्ट्रपति के रूप में उम्मीदवार चुना है लेकिन वैंस की हिंदू पत्नी की धार्मिक पहचान पर उनकी पार्टी चुप्पी साधे हुए है.
उषा चिलुकुरी वैंस अपने मांस और आलू पसंद करने वाले पति, जेम्स डेविड वैंस से बहुत प्यार करती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार जेडी वैंस की पत्नी उषा वैंसने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में दिए भाषण में बताया कि कैसे उनके पति ने उनकी शाकाहारी डाइट को अपनाया और उनकी प्रवासी मां से भारतीय खाना बनाना सीखा। उनके श्वेत, ईसाई पति का दक्षिण भारत के मसालेदार भोजन बनाना, खासकर एक ऐसी पार्टी के नेता के लिए असामान्य है, जिसके अधिकांश सदस्य अभी भी श्वेत और ईसाई हैं।
पारंपरिक रूप से तो भारतीय आप्रवासियों को अमेरिका में डेमोक्रैटिक पार्टी का समर्थक माना जाता है लेकिन उषा वैंस की मौजूदगी ने कुछ भारतीय अमेरिकी दक्षिणपंथियों में उत्साह जगाया है, खासकर हिंदू अमेरिकियों में। लेकिन पिछले महीने मिलवॉकी में दिए गए उनके चार मिनट के भाषण में, उन्होंने अपने हिंदू धर्म और निजी आस्था के बारे में कुछ नहीं कहा।
कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उनका हिंदू अमेरिकी होना अभी भी समुदाय के लिए गर्व की बात है, जबकि अन्य सवाल उठाते हैं कि क्या रिपब्लिकन पार्टी एक ‘हिंदू सेकंड लेडी’ के लिए वास्तव में तैयार है।
धर्म पर उषा वैंस की चुप्पी
उषा वैंस ने चुनाव से पहले अपने धर्म के बारे में चुप्पी साधी हुई है और इस पर एसोसिएटेड प्रेस से बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस बारे में सवालों का जवाब नहीं दिया कि क्या वह हिंदू धर्म का पालन करती हैं या कैथोलिक पति के साथ चर्च जाती हैं, या उनके तीन बच्चों को किस धर्म के तहत पाला जा रहा है।
सैन डिएगो में प्रोफेसर प्रवासी माता-पिता के हिंदू घर में पली-बढ़ी उषा वैंस ने पुष्टि की कि उनके बच्चों में से एक का भारतीय नाम है, और उनकी और जेडी वैंस की शादी भारतीय और अमेरिकी दोनों तरीकों से हुई थी। इन दोनों की मुलाकात येल लॉ स्कूल में पढ़ाई के दौरान हुई थी।
उषा वैंस की हिंदू पृष्ठभूमि कुछ दक्षिण एशियाई मतदाताओं को आकर्षित कर सकती है, जो डॉनल्ड ट्रंप के लिए एरिजोना, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलाइना जैसे स्विंग राज्यों में फायदेमंद हो सकता है, जहां बड़े दक्षिण एशियाई समुदाय हैं। डेनवर यूनिवर्सिटी में हिंदू स्टडीज की प्रोफेसर दीपा सुंदरम कहती हैं कि कुछ भारतीय और हिंदू दक्षिणपंथी उषा वैंस को गले लगाने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि यह पार्टी की सार्वजनिक रणनीति का हिस्सा है।
उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि उनकी हिंदू पहचान पार्टी के लिए फायदे के बजाय एक बोझ है। ऐसा भी लगता है कि अभियान दोनों तरह से लाभ उठाना चाहता है- उषा शायद हिंदू हों, जो कि अच्छी बात है, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते।
सुंदरम ने कहा कि उषा वैंस खासकर उन हिंदू अमेरिकियों को आकर्षित करेंगी जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का समर्थन करते हैं, जिनके तहत हिंदू राष्ट्रवाद का उभार हुआ है।
कुछ भारतीय अमेरिकी समुदायों के भीतर टैक्स, शिक्षा, भारत के साथ संबंध और जाति-विरोधी भेदभाव कानून जैसे मुद्दों पर गहरे मतभेद हैं, जो सिएटल और कैलिफॉर्निया में जोर पकड़ रहे हैं। जाति, जन्म या वंश के आधार पर लोग विभाजित हैं और संबंधित भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करने के लिए अमेरिका में आह्वान बढ़ रहा है।
अब भी डेमोक्रैट हैं अधिकतर भारतीय
प्यू रिसर्च सेंटर के 2022 और 2023 में किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक लगभग 10 में से 7 भारतीयों का झुकाव अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर है जबकि लगभग 3 में से 1 रिपब्लिकन पार्टी के करीबी हैं।
एएपीआई डेटा/एपी-नॉर्क सर्वेक्षणों से इस वर्ष की शुरुआत में पाया गया कि दक्षिण एशियाई अमेरिकियों में से 10 में से एक से भी कम, प्रमुख मुद्दों जैसे गर्भपात, बंदूक नीति और जलवायु परिवर्तन आदि के बारे में रिपब्लिकन पार्टी पर भरोसा करते हैं, जबकि लगभग आधे या अधिक डेमोक्रेटिक पार्टी पर अधिक भरोसा करते हैं।
फिर भी उषा वैंस, एक सेकेंड लेडी जो हमारी तरह दिखती है और हमारी तरह बोलती है, उन मतदाताओं का ध्यान आकर्षित कर सकती हैं, जिन्हें रिपब्लिकन तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है, ऐसा कहना है ओहायो स्टेट सेनेटर नीरज अंटानी का, जो एक रिपब्लिकन और हिंदू अमेरिकी हैं और राज्य सेनेट के सबसे युवा सदस्य हैं।
उन्होंने कहा, अगर रिपब्लिकन अल्पसंख्यक समूहों तक नहीं पहुंचते हैं, तो हम चुनाव हार जाएंगे।
39 वर्षीय बायोटेक उद्यमी विवेक रामास्वामी ने 2020 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था और अब ट्रंप-वैंस का समर्थन करते हैं। उन्होंने पिछले साल जब ट्रंप के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए चुनाव लड़ा तो अभियान के दौरान अपने हिंदू धर्म को प्रमुखता से पेश किया। उन्होंने कहा कि हिंदू शिक्षाएं यहूदी-ईसाई मूल्यों के ही समान हैं। हालांकि वह प्राथमिक चुनाव हार गए थे।
उन्होंने उषा वैंस की धार्मिक पृष्ठभूमि के बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
दक्षिणपंथियों की मजबूत मौजूदगी
बर्कले स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफॉर्निया में शोधकर्ता और एएपीआई डेटा के कार्यकारी निदेशक कार्तिक रामकृष्णन कहते हैं कि उषा वैंस की उनके धर्म पर चुप्पी और रामास्वामी की प्राथमिक चुनाव में हार इस बात का संकेत हो सकती है कि रिपब्लिकन पार्टी के कुछ हिस्सों के लिए ईसाई के अलावा किसी अन्य धर्म का होना अभी भी एक मुद्दा हो सकता है। उन्होंने कहा, कन्वेंशन के बाद हमने रिपब्लिकन पार्टी के भीतर अधिक लोगों को उषा और जेडी वैंस के खिलाफ बोलते देखा है।
इससे मुझे लगता है कि गैर-ईसाई धार्मिक पहचान के बारे में खुला होने की एक राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ती है। अभी लंबा रास्ता तय करना है।
अंटानी ने ओहायो राज्य में चुनाव जीते हैं, जो मुख्यत: ईसाई और बहुत हद तक दक्षिणपंथी राज्य है। अपनी हिंदू पहचान को प्रमुखता से रखने वाले अंटानी कहते हैं, रिपब्लिकन पार्टी में जो नस्लवाद है, वह नस्लवादियों से आ रहा है, ना कि रिपब्लिकन से।
अंटानी ने उषा वैंस द्वारा आरएनसी में अपनी भारतीय विरासत के बारे में बात करने का स्वागत किया। वह मानते हैं कि रामास्वामी की हार इसलिए नहीं हुई क्योंकि वह हिंदू हैं, बल्कि इसलिए कि वह अन्य उम्मीदवारों की तुलना में कम जानकार थे।
कैथोलिक पति की हिंदू पत्नी
जेडी वैंस ने 2019 में कैथोलिक धर्म अपनाया था। वह कहते हैं कि अब वह और उनका परिवार चर्च को अपना घर मानते हैं। उनके प्रचार अभियान दल ने इस बारे में सवालों का जवाब नहीं दिया कि क्या उनके तीन बच्चों ने भी कैथोलिक धर्म अपना लिया है। उन्होंने इस बारे में काफी बात की है कि कैसे उनकी पत्नी ने उन्हें कैथोलिक विश्वास अपनाने में मदद की, जब वह एक आध्यात्मिक यात्रा के दौरान उतार-चढ़ाव का सामना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें प्रोटेस्टेंट के रूप में पाला गया था और कॉलेज में वह नास्तिक बन गए थे।
हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक, सुहाग शुक्ला ने कहा कि उषा वैंस ने अपने पति को कैथोलिक बनने की उनकी धार्मिक यात्रा में प्रेरित किया, यह हिंदू मूल्यों की सबसे बड़ी पहचान है।
उन्होंने कहा, हिंदू धर्म अपने स्वयं के मार्ग को खोजने और अपनी आध्यात्मिकता से जुडऩे के बारे में है। हिंदू की परिभाषा किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो मंदिर जाता है और अनुष्ठान करता है। या फिर ऐसा व्यक्ति जो दिवाली जैसे त्योहार मनाता है या केवल ध्यान जैसी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं तक ही सीमित है।
शुक्ला ने कहा कि उषा वैंस हिंदू अमेरिकियों द्वारा किए गए सकारात्मक योगदान का एक उदाहरण हैं, और उनके अंतरधार्मिक विवाह और विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनने की उनकी क्षमता हिंदू शिक्षाओं की ही पहचान है।
उन्होंने कहा, हिंदू अमेरिकी आत्मसात करते हैं, लेकिन साथ ही वे अपनी परंपरा और संस्कृति से मिली प्रेरणा को भी थामे रहते हैं। हमारी बहुलवादी पृष्ठभूमि हमें विभिन्न लोगों के साथ बिना अपनी पहचान खोए मिल-जुल कर रहने में सक्षम बनाती है। (डॉयचेवैले)
इसराइल में अरसे से प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन होते रहे हैं लेकिन जब इसराइल डिफेंस फोर्स (आईडीएफ़) ने बताया कि उसे शनिवार को दक्षिणी गाजा के रफाह में एक सुरंग में छह बंधकों के शव मिले हैंइसराइली सेना जब तक इन बंधकों तक पहुंच पाती उससे कुछ देर पहले ही इन्हें मार दिया गया था। इसके बाद नेतन्याहू सरकार के खिलाफ हज़ारों की तादाद में लोग सडक़ों पर उतर पड़े।
वहीं छह मृत बंधकों में से एक हेर्श गोल्डबर्ग पोलिन की अंतिम यात्रा यरुशलम में निकली है।
इस दौरान कई शोकाकुलों में से एक शायदना एब्रान्सन ने कहा, हमें माफ कर दो हेर्श हम तुम्हें समय पर नहीं निकाल सके।
सोमवार को इसराइल में सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए आम हड़ताल का आह्वान किया गया लेकिन देश के लेबर कोर्ट ने इसे ख़त्म करने का आदेश दिया।
तेल अवीव की अदालत ने कहा है कि आम हड़ताल अपने समय से पहले ही ख़त्म कर दी जानी चाहिए।
लेकिन आज सुबह से ही देश में ये हड़ताल जारी रही जिसकी वजह से इसराइल में व्यवसायों से लेकर स्कूल और ट्रांसपोर्ट तक ठप पड़ा हुआ है। रविवार को विरोध प्रदर्शन की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से हुई। लेकिन बाद में भीड़ ने पुलिस बैरियर तोड़ दिए और तेल अवीव में प्रमुख हाईवे ब्लॉक कर दिए। प्रदर्शनकारियों ने टायरों में भी आग लगाई।
गज़़ा की एक सुंरग में छह बंधकों के शव मिलने के बाद रविवार से ही हज़ारों लोग सडक़ों पर उतर आए थे। फि़लहाल 97 ऐसे लोग गाजा में हैं जिनके बारे में कोई सूचना नहीं है।
सोमवार की हड़ताल कितनी व्यापक?
इसराइल के लेबर कोर्ट द्वारा हड़ताल रोकने के आदेश से पहले ही कार्यकर्ताओं ने देश के कई हिस्सों में हड़ताल से जुड़े प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है।
देश के कई मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक अवरुद्ध हुआ है। तेल अवीव के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी कुछ फ़्लाइट रद्द हुईं और कई देर से उड़ीं। कई अस्पतालों में सेवाएं बाधित रहीं और बैंक भी बंद रहे।
लेबर कोर्ट के हड़ताल बंद करने के आदेश से पहले तेल अवीव की सडक़ों पर हज़ारों लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया है। इस हड़ताल को इसराइल की सबसे ताक़तवर ट्रेड यूनियन - हिस्ताद्रुत ने बुलाया था।
गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों के संगठन ने आज रात प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के अलावा कई जगहों पर प्रदर्शन करने का एलान किया है।
प्रदर्शनकारी तेल अवीव, यरूशलम और अन्य कई शहरों में इसराइली झंडा अपने हाथों में लेकर निकले।
इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौता करने के लिए पर्याप्त क़दम नहीं उठा पाई है।
इनकी मांग है कि नेतन्याहू की सरकार को बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौता करना चाहिए ताकि हमास की कैद में शेष बंधकों की रिहाई सुनिश्चित हो सके।
इसराइल की ट्रेड यूनियन ने सोमवार को देशव्यापी हड़ताल की जिसे बाद में लेबर कोर्ट ने ख़त्म करने का आदेश दिया। इसराइल के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन के नेता का कहना है कि उनके देश को डील के बजाय शवों के थैले मिल रही हैं।
हड़ताल का असर
सोमवार को आम हड़ताल बुलाने वाली हिस्ताद्रुत ट्रेड यूनियन में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के महानिदेशक पीटर लर्नर ने बीबीसी से कहा कि हड़ताल के कारण पहले से ही कई सेवाओं में रुकावट आई है।
उन्होंने कहा, हम बेन गुरियन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सूटकेसों का अंबार देख रहे हैं। कुछ बंदरगाह अपनी गतिविधियों को कम कर रहे हैं। कुछ नगरपालिकाओं में हम उम्मीद करते हैं कि निजी क्षेत्र में आज व्यवसाय नहीं खुलेंगे।
अदालत के हड़ताल ख़त्म करने के आदेश से पहले बेन गुरियन हवाई अड्डे पर कुछ उड़ानें स्थगित हुई हैं।
ग्रीस जा रहे ज़मी मोल्दोवन ने कहा, हमें पता चला कि ग्रीस के लिए हमारी उड़ान स्थगित कर दी गई है। मैं इस हड़ताल का समर्थन करता हूँ क्योंकि वास्तव में इसराइल के सभी लोग चाहते हैं कि हमारे दोस्त और भाई गज़ा से आज़ाद हों और लौटें।
हवाई उड़ानों पर तो असर पड़ा ही है, काम धंधे और स्कूल पर भी हड़ताल का असर है। हाइफा में रामबाम अस्पताल में सर्जरी विभाग के प्रमुख, प्रोफेसर येहुदा उल्मन ने कहा कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया।
प्रोफ़ेसर येहुदा उल्मन ने बताया, हम हड़ताल पर हैं। यह उन डॉक्टरों के लिए बहुत कठिन शब्द है जो रोगियों के जीवन और कल्याण की देखभाल करने के लिए यहां हैं। लेकिन हम और पूरा देश अब बहुत ही कठिन स्थिति में हैं, बंधकों की वजह से। और कल शायद यह सबसे कठिन दिन था क्योंकि हमने उन छह बंधकों के बारे में सुना जो ग्यारह महीने तक पीड़ा सहने के बाद मारे गए। हम अलग नहीं रह सकते और इसलिए हमने हड़ताल की।
पिछले साल सात अक्टूबर को इसराइल पर हमास ने हमला किया था और इसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों को बंधक बनाकर गज़़ा ले जाया गया था।
बंधकों की रिहाई को लेकर सरकार पर दबाव
इसराइली बंधकों के परिवारों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल में हिस्सा लिया। शेरोन लिफ्शित्ज़ लंदन में एक फि़ल्म निर्माता और शिक्षाविद हैं।
हमास ने 7 अक्टूबर को जिन लोगों को बंधक बनाया था उनमें उनके माता-पिता भी थे। उनकी माँ तो नवंबर के युद्ध विराम के दौरान रिहा हो गईं, लेकिन उनके 83 साल के पिता अभी भी लापता हैं।
माना जाता है कि उन्हें गज़़ा में बंदी बनाकर रखा गया है। उनका कहना है कि जब तक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते, बंधकों की जान जोखिम में है।
शेरोन कहते हैं, ये बंधक एक हफ़्ते से भी कम समय पहले तक जिंदा थे। वे इसलिए मारे गए क्योंकि समझौते पर हस्ताक्षर करने में देरी हो रही है। इसराइल सरकार और हमास इस समझौते तक पहुँचने के रास्ते में और भी अड़चनें डाल रहे हैं।
मुझे और यहाँ रहने वाले समझदार नागरिकों को उम्मीद है कि इन मौतों के कारण पूरी दुनिया में हंगामा मचेगा, जिससे इसराइल और हमास की सरकारें इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होंगी और इस भयानक घटना का अंत होगा।
शेरोन का कहना है कि गज़़ा में अपने सैन्य अभियान के ज़रिए हमास को हराने की इसराइली सरकार की प्रतिज्ञा काम नहीं आएगी।
शेरोन की तरह ही जोनाथन डेकेल-चेन के पिता अभी भी बंधक हैं। उन्होंने दोहराया कि वह युद्धविराम और बंधकों के लिए एक समझौता चाहते हैं।
जोनाथन डेकेल-चेन कहते हैं, प्रधानमंत्री नेतन्याहू और याह्या सिनवार दोनों की जो सोच है वो साफ़तौर पर ज़मीनी हकीकत नहीं बयान करते हैं। उन्हें खुद के राजनीतिक या वैचारिक एजेंडे को अलग रखना होगा और लोगों की भलाई के लिए युद्ध विराम और बंधक समझौते पर पहुंचने के लिए तेजी से काम करना होगा। जब तक वे दोनों यह तय नहीं कर लेते कि उनका अपना राजनीतिक भविष्य या वैचारिक मसीहावाद उनके अपने लोगों की सुरक्षा से कम महत्वपूर्ण है।
समझौते में देरी क्यों?
बंधकों की रिहाई पर समझौता ना हो पाने के लिए इसराइल के प्रधानमंत्री बिनयामिन नेतन्याहू ने हमास नेताओं को दोषी ठहराते हुए कहा है कि हत्याओं से पता चलता है कि वे कोई समझौता नहीं चाहते थे।
नेतन्याहू का कहना है कि दिसंबर से हमास वास्तविक वार्ता करने से मना कर रहा है। तीन महीने पहले, 27 मई को, इसराइल ने अमेरिका के पूरे समर्थन के साथ बंधक रिहाई समझौते पर सहमति जताई थी। हमास ने इस दावे से इंकार किया है।
नेतन्याहू का कहना है, अमेरिका के 16 अगस्त को मसौदे की रूपरेखा को अपडेट करने के बाद भी हम सहमत हुए और हमास ने फिर से इंकार कर दिया। इस समय भी, जब इसराइल एक समझौते पर पहुंचने के लिए मध्यस्थों के साथ गहन वार्ता कर रहा है, हमास का किसी भी प्रस्ताव को खारिज करना जारी है। इससे भी बदतर बात ये है कि जारी वार्ता के दौरान उसने हमारे छह बंधकों की हत्या कर दी। जो बंधकों की हत्या करता है वह समझौता नहीं चाहता है।
ताज़ा घटनाक्रम के बाद नेतन्याहू ने कहा इसराइल हमास के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा।
लेकिन नेतन्याहू सिर्फ आम लोगों के ही निशाने पर नहीं हैं, उन्हें विपक्ष के हमलों का भी सामना करना पड़ा है।
विपक्ष के नेता याएर लैपिड ने नेतन्याहू पर बंधकों को न बचाने का फैसला करने का आरोप लगाया है।
लैपिड ने कहा है, वे जि़ंदा थे। नेतन्याहू और मौत की कैबिनेट ने उन्हें ना बचाने का फैसला किया। अभी भी जीवित बंधक हैं, अभी भी कोई समझौता हो सकता है। नेतन्याहू राजनीतिक वजहों से ऐसा नहीं करना चाहते। उन्हें हमारे बच्चों की जि़ंदगी बचाने के बजाय बेन-ग्विर के साथ गठबंधन को बचाना पसंद है। इन हत्याओं का दोष उनके सिर माथे रहेगा। (bbc.com/hindi)
- दिलीप कुमार शर्मा
24 साल के असम के राजीबुल हक़ नाराजगी और हताशा से सवाल पूछते हैं, क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं, हमारी हिफाजत कौन करेगा?
वो अपनी आपबीती बताते हैं, हम लोग रोज़ी रोटी के लिए काम करने ऊपरी असम गए थे। तीन साल से चराईदेव के धोलेबाग़ान में काम कर रहे थे। लेकिन उस रात मुंह पर कपड़ा बांधे 14-15 लोग वहां आ गए, उनके पास हथियार थे।
उन्होंने हमें बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। आखऱि हमारा कसूर क्या था? पीठ पर पाइप और डंडों से इतना मारा कि अब तक मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूं। क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं?
राजीबुल तीन साल से बतौर राजमिस्त्री असम सरकार की एक योजना के तहत चराईदेव में निर्माण हो रहे तीन मंज़िला कौशल विकास केंद्र में काम रहे थे।
चराईदेव असमिया बहुल ऊपरी असम का एक जिला है, जहां पिछले कुछ दिनों से असमिया जातीय संगठनों ने मियां मुसलमान यानी बंगाली मूल के मुसलमानों को इलाके़ से चले जाने की चेतावनी जारी कर रखी है।
राजीबुल और उनके साथ काम करने वाले आठ मज़दूर साथियों की शिकायत के बाद बारपेटा पुलिस ने निर्माण कार्य के ठेकेदार मयूर बोरगोहाईं के खिलाफ एक जीरो एफआईआर दर्ज कर ली है।
मयूर बोरगोहाईं शिवसागर जिले के बीजेपी अध्यक्ष हैं और 2021 में नाजिरा विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। बारपेटा सदर थाने के प्रभारी के.नाथ ने बीबीसी से कहा, हमने नौ मजदूरों की शिकायत के बाद एक जीरो एफआईआर दर्ज की है। सभी मजदूरों का मेडिकल चेकअप करवा लिया गया है और उनका बयान दर्ज किया गया है। हमने इस एफआईआर को चराईदेव जिले के मथुरापुर थाने में भेज दिया है।
मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर
इन सबके बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाले 18 विपक्षी दलों के संयुक्त मंच ने प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज कराई है।
यह एफआईआर बुधवार (28 अगस्त) को गुवाहाटी के दिसपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है जिसमें मुख्यमंत्री सरमा पर धर्म और जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश करने के आरोप लगाए गए हैं।
इसके साथ ही यूनाइटेड ऑपोज़िशन फोरम ने भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी भेजा है जिसमें मुख्यमंत्री सरमा को बर्खास्त करने की मांग की गई है।
विपक्षी दलों का आरोप है कि बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री सरमा ने ख़ासकर मियां मुसलमानों को लेकर जिस तरह के बयान दिए हैं इसके परिणामस्वरूप राज्य में सांप्रदायिक माहौल पैदा हो गया है।
चराईदेव में मुस्लिम मजदूरों की पिटाई के मामले को भी इससे जोड़ कर देखा जा रहा है।
बीते शनिवार (24 अगस्त) की रात कऱीब साढ़े 10 बजे निर्माण स्थल पर हुए हमले के बारे में राजीबुल कहते हैं, हमने शिवसागर में मियां मुसलमानों के खिलाफ चेतावनी जारी करने की न्यूज देखी थी। इसलिए शनिवार को हम लोगों ने ठेकेदार मयूर बोरगोहाईं से बकाया पैसा मांगा था। उन्होंने पैसा देने की बात भी कही लेकिन रात को उन लोगों ने हमारी पिटाई कर दी।
हमारे ठेकेदार बीजेपी के नेता हैं और उन्होंने मियां लोगों को जो धमकी जारी की थी उसकी आड़ में हमें पिटवाया ताकि हम पैसा लिए बगैर डरकर वहां से भाग जाएं। राजीबुल ने बारपेटा लौटकर मयूर बोरगोंहाईं के ख़िलाफ़ जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें 15 लाख रुपए बक़ाया होने की बात भी कही गई है।
पिटाई वाली रात की घटना को याद करते हुए 18 साल के एक और मजदूर आहादुल खान कहते हैं, उस रात को मैं कभी नहीं भूल सकता। एक पल के लिए तो लगा कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। वहां 15 लोग आए थे। दो लोगों के हाथों में पिस्तौल भी थी। कुछ लोग छुरा लिए हुए थे और कुछ लोगों के हाथ में फावड़े और डंडे थे। उन लोगों ने हमें कान पकड़ कर घुटने के बल बैठने के लिए कहा और डंडों से मारना शुरू कर दिया।
आहादुल ख़ान कहते हैं कि उनसे इलाका छोडक़र जाने के लिए कहा गया।
उन्होंने बताया, हम 15 मुस्लिम मजदूर थे। वो लोग हमें पीटे जा रहे थे और एक व्यक्ति पिटाई का वीडियो बना रहा था। वो जिस तरह के नारे लगाने के लिए कह रहे थे हम वैसा ही कर रहे थे। उन लोगों ने एक घंटे तक हमारी पिटाई करने के बाद हमें तुरंत इलाक़ा छोडक़र चले जाने को कहा। उन लोगों ने कहा आधे घंटे बाद हम फिर आएंगे। इस घटना को लेकर असम में बंगाली मूल के मुसलमान समुदाय में काफी नाराजगी है।
मजदूरों की पिटाई से नाराज बारपेटा जिले के मुस्लिम नेता अलामिन हक ने कहा, भारत का नागरिक होने के नाते हम कामकाज के लिए हर जगह आ-जा सकते हैं। सरकार से हमारा अनुरोध है कि जिसने भी निर्दोष मजदूरों पर हमला किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।
कैसे शुरू हुआ विवाद?
दरअसल 13 अगस्त को ऊपरी असम के शिवसागर शहर में एक नाबालिग असमिया लडक़ी पर कथित रूप से हमला करने की घटना सामने आई थी। इस हमले के अभियुक्तों की पहचान मारवाड़ी समुदाय के स्थानीय व्यापारियों के रूप में की गई थी।
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन इससे नाराजगी कम नहीं हुई।
इस घटना ने शहर में गैऱ-असमिया निवासियों ख़ासकर गैऱ-असमिया व्यापारियों के खिलाफ जातीय संगठनों में आक्रोश की लहर पैदा कर दी।
मामला बढ़ा और एक स्थानीय लडक़ी पर इस तरह हमले को लेकर 30 असमिया राष्ट्रवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके परिणामस्वरूप गैऱ-असमिया लोगों के स्वामित्व वाली दुकानों और व्यवसायों को बंद कर दिया गया।
इस विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य के कैबिनेट मंत्री रनोज पेगु और जिला प्रशासन के अधिकारियों और मीडिया की मौजूदगी में मारवाड़ी समुदाय के पुरुष और महिला प्रतिनिधियों ने प्रदर्शनकारी संगठनों के सामने घुटने टेककर सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी।
लेकिन राजस्थान मूल के लोगों के माफ़ी मांगने का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ सोशल मीडिया पर लोगों ने सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया।
कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए कि देश में कानून व्यवस्था के होते हुए इस तरह किसी को घुटने पर बैठा कर मंत्री और प्रशासन की मौजूदगी में माफी मांगने के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता है।
जिस वक्त राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मामला तूल पकड़ रहा था, लगभग उसी वक्त नगांव जिले के धींग में एक नाबालिग असमिया लडक़ी के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आ गई।
22 अगस्त को इस घटना में जिन तीन युवकों पर आरोप लगे उनका नाता बंगाली मूल के मुसलमान समुदाय से है। इसके बाद इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जो बयान दिया कुछ लोग उसे सांप्रदायिक बता रहे हैं।
इस कथित बलात्कार की घटना के बाद मुख्यमंत्री सरमा ने 23 अगस्त को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जिन अपराधियों ने धींग की एक हिंदू नाबालिका के साथ जघन्य अपराध करने का साहस किया, उन्हें कानून छोड़ेगा नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद एक विशेष समुदाय अत्यंत सक्रिय हो रहा है। हिंदुओं को भाषाओं के आधार पर बांटने की कोशिश से सभी को सतर्क रहना चाहिए।
इसके बाद जब यह मामला असम विधानसभा में उठा तो बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सदन में कहा कि वह पक्ष लेंगे और मियां मुसलमानों को राज्य पर क़ब्जा नहीं करने देंगे।
हिमंत की नीति को लेकर असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया कहते हैं, ऊपरी असम के जोरहाट लोकसभा सीट पर जब से गौरव गोगोई जीते हैं मुख्यमंत्री परेशान हैं क्योंकि उन्होंने गौरव गोगोई को सबसे ज़्यादा वोटों से हराने की चुनौती दी थी। लेकिन गौरव गोगोई एक लाख 44 हज़ार वोटों से जीत गए।
अब मुख्यमंत्री ऊपरी असम में वोटरों को खुश करने के लिए नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं। हिंदी भाषी समुदाय के जिन लडक़ों ने गलत काम किया था, उनके खिलाफ पुलिस को समय पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। जब मामला बहुत बढ़ गया तो सीएम ने अपने एक कैबिनेट मंत्री को भेजा जनकी मौजूदगी में हिंदी भाषी लोगों को घुटनों पर बैठाकर माफ़ी मंगवाई गई।
कांग्रेस नेता सैकिया कहते है, लेकिन हिंदी भाषी समुदाय के मुद्दे पर ज़रूर दिल्ली से सीएम को डांट पड़ी होगी, तो फिर उनका दिमाग घूम गया। क्योंकि समूचे देश में हिंदी भाषी लोग बीजेपी के वोटर हैं। जब यह तरीका भी काम नहीं आया तो उन्होंने धार्मिक आधार पर राजनीति का खेल खेलना शुरू कर दिया ताकि ऊपरी असम में कांग्रेस को बैकफुट पर ले जा सकें।
दरअसल निचले असम में बंगाली मूल के मुसलमानों की एक बड़ी आबादी बसी है जिनकी नागरिकता को लेकर असम में राजनीति होती रही है।
हालांकि अपने इन आक्रामक बयान के दो दिन बाद सीएम सरमा ने कहा कि भारत हम लोगों की जन्मभूमि है और हम इस देश में टैक्स देते हैं, इसलिए सभी नागरिक किसी भी जगह आ-जा सकते है।
विपक्षी दलों ने स्थानीय पुलिस से अनुरोध किया कि वह सीएम हिंमत बिस्वा सरमा और उनके सह-षडय़ंत्रकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 61, 196 और 35 (2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू करें। हालांकि पुलिस ने विपक्ष की इस एफआईआर के तहत अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है।
दिसपुर पुलिस थाने के प्रभारी रूपम हजारिका ने बीबीसी से कहा, यूनाइटेड ओपोजशिन फोरम से हमें एक शिकायत मिली है, लेकिन अभी मामला रजिस्टर नहीं किया गया है। फिलहाल आरोपों की जांच की जा रही है।
नागरिकता के मुद्दे को सुलझाने में
केंद्र की सरकारें नाकाम रहीं
असम में लगभग तीन दशकों से पत्रकारिता कर रहे नव कुमार ठाकुरिया की मानें तो राज्य में बाहरी और स्थानीय लोगों के बीच टकराव और पूर्वी पाकिस्तान से आए लोगों के मुद्दे का समाधान किसी भी सरकार ने नहीं किया। लिहाजा अब यह टकराव ऊपरी सतह पर गया है।
वो कहते है, पूर्वी पाकिस्तान से जब 1971 में बांग्लादेश को अलग करने के लिए युद्ध हुआ तो भारत की सेना ने वो युद्ध जीतकर दिया। पाकिस्तानी सेना ने भारत की सेना के समक्ष समर्पण किया था न कि बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं के सामने। उस दौरान हजारों बांग्लादेशी असम और पूर्वी भारत में घुस आए थे। उनका बोझ असम के लोगों पर पड़ा। उस समय की सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए।
जब 1985 में असम समझौता हुआ तो उस पर न तो प्रधानमंत्री ने कोई हस्ताक्षर किए न ही असम के मुख्यमंत्री ने। वो समझौता मूल रूप से नौकरशाही के साथ हुआ था। असम समझौते को लेकर संसद में कभी कोई बहस नहीं हुई। लिहाजा यह समस्या आज तक असम के लोगों को चिंता में डाले हुए है। उसी को लेकर टकराव अब भी जारी है।
असम की मौजूदा राजनीति की बारीकियों को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक बैकुंठ नाथ गोस्वामी की मानें तो धुबड़ी लोकसभा सीट से एआईयूडीएफ़ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल की हार से बीजेपी का राजनीतिक गणित बदल गया है।
वो कहते हैं, अब तक अजमल की राजनीति से बीजेपी को ध्रुवीकरण का फायदा मिल रहा था लेकिन धुबड़ी सीट में 10 लाख से ज़्यादा वोटों से अजमल की हार से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि निचले असम में अजमल का जो वोट बैंक था वो कांग्रेस की तरफ चला गया।
वहीं ऊपरी असम में गौरव गोगोई जीत गए। लिहाजा अब हिंदू वोटरों को एक साथ लाने के लिए बीजेपी ने इस तरह की भावनात्मक राजनीति शुरू कर दी है। धींग की घटना की आड़ में मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है वो इसी राजनीति का हिस्सा है।
बीजेपी का जवाब
लेकिन बीजेपी खुद पर लग रहे ध्रुवीकरण की कोशिशों के आरोपों से इनकार करती है।
असम प्रदेश बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद स्वामी का कहना है उनकी पार्टी के किसी भी नेता ने कोई सांप्रदायिक बयानबाजी नहीं की है।
वो कहते हैं, बीते कुछ दिनों से राज्य में बलात्कार की कुछ घटनाएं सामने आ रही थीं। खासकर धींग में नाबालिग लडक़ी के साथ जो घटना हुई और उसके बाद जो राज्य का एक माहौल था।। उससे लोगों में काफी गुस्सा है।
असम में अवैध घुसपैठ की समस्या काफी पुरानी है लिहाजा ऊपरी असम के कुछ संगठनों के विरोध के बाद तनाव पैदा हो गया। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि अभी निचले असम के लोगों को ऊपरी असम नहीं जाना है क्योंकि कानून-व्यवस्था को बनाए रखना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है।
उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति के सवाल पर कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने हाल के लोकसभा चुनाव में असम की 14 में से 11 लोकसभा सीटें जीती हैं।
उन्होंने कहा, ऊपरी असम में जोरहाट के अलावा भी कई सीटें बीजेपी ने जीती हैं, लिहाजा विपक्ष को अपना गणित सुधारने की ज़रूरत है। (bbc.com/hindi)
-रेहान फजल
राजनीति और समाज पर परसाई की पकड़ इतनी गहरी थी कि आज उनके गुजर जाने के बरसों बाद भी नए जमाने में सोशल मीडिया पर उनके लिखे वाक्य हर तरफ नजर आते हैं।
किसी और दौर में लिखी परसाई की हर चुटीली बात ऐसी लगती है मानो वह बिल्कुल ताजा हालात को देखकर लिखी गई है।
एक बार जाने-माने लेखक कमलेश्वर ने परसाई के बारे में कहा था, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने जो भी पत्रिकाएं संपादित कीं उनमें से कोई भी परसाई के कॉलम के बगैर छपी नहीं क्योंकि मुझे लगता था कि जो मैं तमाम रचनाओं के माध्यम से नहीं कह पाऊँगाा, जो मैं संपादकीय के माध्यम से नहीं कह पाऊँगाा, वो मैं परसाई की एक रचना के माध्यम से कह लूँगा इसीलिए मैंने हमेशा परसाई से पहले बात की और पत्रिका का संपादक बाद में बना।
परसाई के लिखे स्तंभ ऐसे होते थे कि वो वाकई किसी पत्रिका के ‘स्तंभ’ बन जाया करते थे। उस पर खड़ी कोई भी पत्रिका स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती थी।
1970-1980 के दशक में धर्मयुग हिंदी की सबसे लोकप्रिय पत्रिका हुआ करती थी।
राजेंद्र चंद्रकांत राय हरिशंकर परसाई की जीवनी ‘काल के कपाल पर हस्ताक्षर’ में लिखते हैं, परसाई धर्मयुग मे हर महीने छपते थे और कभी-कभी तो महीने में दो बार भी। वैचारिक रूप से परसाई न तो धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती के अनुकूल थे और न ही धर्मयुग को छापने वाली कंपनी बेनेट कोलमैन के। पर वे पाठकों के मन के अनुकूल जरूर होते थे।
कमलेश्वर ने लिखा भी है, जब भी सारिका में परसाई का स्तंभ शुरू होता था, सारिका का प्रिंट ऑर्डर बढ़ जाता था। परसाई जी हिंदी साहित्य के दिलीप कुमार थे।
जाने-माने व्यंग्यकार रवींद्रनाथ त्यागी ने बिल्कुल सही कहा था, आज़ादी से पहले के हिंदुस्तान जानने के लिए जैसे सिफऱ् प्रेमचंद पढऩा ही काफ़ी है, उसी तरह आज़ादी के बाद का पूरा दस्तावेज़ परसाई की रचनाओं में सुरक्षित है।
कबीर के मुरीद
परसाई ने अपने समय की सच्चाइयों को लोगों के सामने रखने के लिए व्यंग्य को माध्यम बनाया। बीमार व्यवस्था को बदलने की बेचैनी उनमें थी।
वो हिंदी पट्टी के नायक बने और फिर सितारा हुए। वो कबीर के बखियाउधेड़ फक्कड़पन के मुरीद थे।
सन् 1974 से 1976 तक उन्होंने सारिका पत्रिका में ‘कबिरा खड़ा बाज़ार’ शीर्षक से एक स्तंभ लिखा जिसमें उन्होंने साक्षात्कार शैली का इस्तेमाल किया। इसमें परसाई कबीर की तरफ से देश-विदेश के नामी राजनेताओं और महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों से काल्पनिक इंटरव्यू लिया करते थे।
सन् 1975 में आपातकाल लगा और उसी वर्ष के सारिका के जून अंक में बाबू जगजीवन राम से ‘कबीर’ का साक्षात्कार छपा था। इसमें जगजीवन राम ने कबीर से कहा था, ‘अगर जयप्रकाश नारायण का सरकार बनाना पक्का हो जाए तो मैं उनकी तरफ़ चला जाऊँ।’
सेंसर वालों ने इस अंक की दुर्गति कर दी थी। आधे पन्ने काले करने पड़े। दिलचस्प बात ये थी कि करीब डेढ़ साल बाद जगजीवन राम वाकई कांग्रेस छोडक़र जयप्रकाश नारायण से जा मिले थे। परसाई 16 और 32 पेज वाली कॉपियों पर अपने लेख लिखा करते थे।
बाद में वो बोलकर भी लिखवाने लगे थे। उनके जीवनीकार राजेंद्र चंद्रकांत राय लिखते हैं, डॉक्टर राम शंकर तिवारी उनके नज़दीक रहते थे। ज़्यादातर वही उनका डिक्टेशन लेते थे। फिर वही कॉपी संपादकों को डाक से भेज दी जाती थी। मेरे लिए अचरज वाली बात ये थी कि उसकी कॉपी अपने पास नहीं रखते थे।
सब पर थी परसाई की पैनी नजरें
पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह पर केंद्रित एक स्तंभ ‘संन्यासी की वापसी’ का मज़ा लीजिए में वो लिखते हैं, ‘‘चर्चिल के बारे में कहा जाता है कि वो जहाँ जाते थे, वहाँ सबके ध्यान के केंद्र होना चाहते थे। वो अगर बारात में जाएं तो दूल्हा होना चाहेंगे और शव यात्रा में जाएं तो लाश होना चाहेंगे। ऐसा ही अपने चौधरी साहब का व्यक्तित्व है इसलिए उन्होंने कह दिया कि विपक्षी एकता में अगर मैं प्रधानमंत्री बना दिया जाऊँ तो मैं अपना संन्यास छोड़ता हूँ।
‘ये माजरा क्या है’ स्तंभ में परसाई ‘डॉक्टरेट की कथा’ शीर्षक लेख में लिखते हैं, ‘फ्ऱांस में डॉक्टरेट बहुत सस्ती हो गई थी। कोई 500 फ्ऱैंक विश्वविद्यालय को भेज दे और मनचाहे विषय पर डॉक्टरेट ले ले। एक रईस ने 8-10 विषयों पर डॉक्टरेट ले ली। वो अपने घोड़े को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी को 500 फ्ऱैंक भेजे और लिखा कि मेरे घोड़े को भी एक डॉक्टरेट दे दी जाए। जवाब आया, हम घोड़ों को डॉक्टरेट नहीं देते, सिफऱ् गधों को देते हैं।’
कपिल कुमार सिंह राघव अपनी किताब ‘हरिशंकर परसाई का व्यंग्य साहित्य’ में लिखते हैं, ‘हिंदी में स्तंभ लेखन के माध्यम से अपने मन की बातें जितनी परसाई ने कहीं किसी अन्य ने इतने तीक्ष्ण रूप में नहीं कहीं। कोई समाज, कोई राज्य, कोई राष्ट्र परसाई की नजऱों से बचा नहीं है। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर पढ़े-लिखे समुदाय को अपने आसपास की सच्चाई के बारे में सजग किया है।’
प्लेग में माँ को खोया
स्वाभाविक है कि परसाई के पाठकों को इसमें दिलचस्पी हो कि वो जो इतना हँसते और हँसाते हैं, जिसमें मस्ती है, जो ऐसे तीखे हैं, कटु हैं। इनकी अपनी जि़ंदगी कैसी रही?
परसाई सारिका में प्रकाशित अपने आत्मकथ्य ‘गर्दिश के दिन’ में लिखते हैं कि उनके बचपन की सबसे तीखी याद प्लेग की है। 1936 या 37 रहा होगा। तब वे आठवीं के छात्र थे। प्लेग के कारण कस्बे की सारी आबादी घर छोडक़र जंगल में टपरे बनाकर रहने चली गई थी। वे नहीं गए थे क्योंकि उनकी माँ सख़्त बीमार थीं। उन्हें लेकर जंगल नहीं जाया जा सकता था।
परसाई ने लिखा है, भाँय-भाँय करते पूरे इलाके में हमारे घर पर चहल पहल थी। कुत्ते तक बस्ती छोड़ गए थे। रात के सन्नाटे में हमारी आवाज़ें हमें ही डरावनी लगती थीं। रात को मरणासन्न माँ के सामने हम लोग आरती गाते। गाते-गाते पिताजी सिसकने लगते। माँ बिलखकर हम बच्चों को सीने से लगा लेतीं। हम भी रोने लगते।
आत्मकथ्य में उन्होंने लिखा है, रात को पिताजी, चाचा और दो एक रिश्तेदार बल्लम लेकर घर के चारों तरफ़ घूम-घूम कर पहरा देते। वो सब नहीं जानते थे कि वो पहरेदारी किससे कर रहे हैं? चोरों सेज्? डकैतों सेज्? या आसन्न मृत्यु से।।।? ऐसे भयानक वातावरण में एक रात तीसरे पहर माँ की मृत्यु हो गई। प्लेग की वो रातें मेरे मन में गहरे उतरी हैं। जिस आतंक, अनिश्चय, निराशा और भय के बीच में हम जी रहे थे उसके सही अंकन के लिए बहुत पन्ने चाहिए।
व्यंग्य लेखक का जन्म
परसाई के जीवन में सब कुछ अंधकारमय नहीं था। उसमें मस्ती भी थी और बेफिक्री भी।
‘गर्दिश के दिन’ में ही परसाई लिखते हैं, ‘एक विद्या मुझे आ गई थी, वो थी बिना टिकट सफऱ करना। जबलपुर से इटारसी, खंडवा, देवास बार-बार चक्कर लगाने पड़ते। पैसे थे नहीं। मैं बिना टिकट बेखटके गाड़ी में बैठ जाता। बचने की बहुत तरकीबें आ गई थीं। पकड़ा जाता तो अच्छी अंग्रेजी में अपनी मुसीबत का बखान करता। टिकट चेकर प्रभावित हो जाते और कहते, ‘लेट्स हेल्प द पुअर ब्वॉय।’
परसाई लिखते हैं, ‘इन गर्दिशों का जि़क्र आखऱि मैं क्यों विस्तार से कर गया? गर्दिशें बाद में भी आईं। अब भी आती हैं लेकिन उस उम्र की गर्दिशों की अपनी अहमियत है। लेखक की मानसिकता और व्यक्तित्व निर्माण से इसका गहरा संबंध है। मैंने सोचा दुखी और भी हैं। अन्याय पीडि़त और भी हैं। अनगिनत शोषित हैं। मैं उनमें से एक हूँ। पर मेरे हाथ में कलम है और मैं चेतना संपन्न हूँ। यहीं कही व्यंग्य लेखक का जन्म हुआ।’
समकालीन साहित्यकारों की चुटकी
परसाई ने लेखन के अलावा अपने समकालीन साहित्यकारों पर बेबाक टिप्पणियाँ की हैं।
वो लिखते हैं, ‘इनका सहज कुछ नहीं होता था। उनके शब्द बनावटी, उन्हें बोलते वक्त होठों के मोड़ बनावटी, आँखों का भाव बनावटी, मुस्कान बनावटी। ये लोग समझते थे कि सब कुछ उनकी कविता और कहानी से हो जाने वाला है। मैं इन्हें देखता था, सुनता था पर पास नहीं जाता था। वे मूर्ति थे, जिन पर फूल चढ़ा सकते थे पर जिनसे बात नहीं कर सकते थे।’
उन दिनों साहित्य का तीर्थ इलाहाबाद हुआ करता था। परसाई वहाँ अक्सर जाते थे।
वो अपनी किताब ‘जाने पहचाने लोग’ में लिखते हैं, ‘मेरी आदत नहीं है कि अगर तीर्थ गए हैं तो हर मंदिर में नारियल फोड़ूँ। अज्ञेय से मेरी आज तक दुआ सलाम नहीं हुई इसका कारण मेरा अहंकार नहीं है, संकोच है। अज्ञेय मुझे चित्र से और सामने से भी एक उदास दार्शनिक लगते हैं। मैं उनसे मिलने जाता तो वो 22वीं सदी के मनुष्य की चिंता में लीन हो जाते। मैं उनसे क्या बात करता? वैसे भी लेखकों से बात करना मेरी लिए कठिन है।’
बेबाक टिप्पणियाँ
परसाई मैथिलीशरण गुप्त से भी कभी नहीं मिले लेकिन उनके बारे में कई दिलचस्प बातें लिखी। उनके बारे में कहा जाता था जब कोई लेखक उनसे मिलने जाता था तो उनके घर के बाहर उनका कोई भाई या भतीजा मिलता था।
परसाई लिखते हैं, ‘वो लेखक से पूछता था, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन-सा है? यदि लेखक ‘कामायनी’ (जयशंकर प्रसाद की रचना) का नाम ले देता और ‘साकेत’ (मैथिलीशरण की रचना) का नहीं तो उसके साथ वहाँ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था।’
इलाहाबाद में ही परसाई को उपेंद्रनाथ अश्क से भी मिलने का कई बार मौका मिला।
परसाई लिखते हैं, ‘अश्क जी से मिलना एक विशिष्ट अनुभव है। अपने को कुछ नहीं बोलना पड़ता। वो ही बोलते हैं और अपने बारे में बोलते हैं। उनके पास बैठने से सबसे बड़ी प्राप्ति ये होती है कि सारे लेखकों की बुराई मालूम हो जाती है और उनकी नई से नई कलंक कथा आप जान जाते हैं। इलाहाबाद में महादेवी जी से भी कई बार भेंट हुई। वो खुलकर बात करती हैं और खुली हँसी हँसती हैं।’
श्रीकांत वर्मा के लिए स्नेह
जैनेंद्र कुमार से भी हरिशंकर परसाई की अक्सर नोकझोंक हुआ करती थी, एक बार दोनों को दिल्ली में एफ्रो-एशियाई शांति सम्मेलन में आमंत्रित किया गया।
परसाई लिखते हैं, जैसे ही जैनेंद्र ने मुझे देखा मुझसे कुटिल मुद्रा में बोले, ‘इस सम्मेलन में आने के लिए तुम्हें रूस से बहुत पैसा मिला होगा।’ मैंने कहा ‘जी हाँ इस सम्मेलन को बिगाडऩे के लिए जितना पैसा सीआईए से आपको मिला है।’ जैनेद्र हंसे और कहने लगे, तुम्हारी कटाक्ष की क्षमता अद्भुत है।
श्रीकांत वर्मा के लिए परसाई के मन में बहुत स्नेह था। उनकी नजऱ में श्रीकांत में बहुत आत्मीयता थी। ऊपर से कटु और ‘एरोगेंट’ लगने वाला ये आदमी भीतर से बहुत कोमल था। परसाई को तभी आभास हो गया था कि श्रीकांत महत्वाकांक्षी है।
परसाई लिखते हैं, ‘मुझे लग गया था कि वो दूसरे क्षेत्रीय कवियों की तरह कवि-सम्मेलनों में कविता पढक़र संतुष्ट नहीं होगा। श्रीकांत मुझसे और मुक्तिबोध से भिन्न था। हम दोनों कस्बे में रह कर भी अपना काम कर लेते थे। श्रीकांत को विराटता चाहिए थी और ‘स्पेस’ भी। वो बहुत अध्ययन करता था। साथ ही वो अपनी अलग तेज़ धारदार भाषा बना रहा था। इस भाषा की कोई नकल नहीं कर सकता था। वो भाषा श्रीकांत के साथ ही चली गई।’
परसाई अपने साथी लेखकों और कवियों को बहुत बारीकी से देखते थे। कुछ कवि तो मंच पर जाने से पहले बाल सँवारते थे लेकिन कुछ कवि ऐसे थे जो इनके सामने खड़े होकर सँवरे हुए बालों को बिखेरते थे। कभी बेहद लोकप्रिय कवि नीरज को परसाई ने बाल बिखराते और बदहवासी का भाव धारण करते देखा था।
शमशेर बहादुर सिंह और नामवर सिंह के प्रशंसक
शमशेर बहादुर सिंह के साथ भी हरिशंकर परसाई की बहुत नजदीकी थी। शमशेर में बहुत नफासत थी। वो काफी अंतर्मुखी थे।
परसाई लिखते हैं, शमशेर की मुस्कान ‘डिसआर्मिंग’ है। वो निहायत संकोची और अपना अधिकार तक छोडऩे वाला आदमी है। नागार्जुन भी कविता में रहते हैं पर व्यवहारिक मामलों में चतुर, चालाक, हिसाबी और अपना हक झपट लेने वाले हैं। शमशेर अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, फ़ारसी और फ्ऱेंच के विद्वान हैं। उर्दू उनकी पहली भाषा है, हिंदी दूसरी। जिस अदा से वो ‘डॉट्स’, ‘हाइफऩ’ और ‘डैश’ के साथ सोचते हैं, वैसा ही लिखते और बोलते भी हैं। ‘एबसेंट माइंडेड’ हो जाना उनकी आदत है।
नामवर सिंह के लिए भी परसाई के मन में ‘सॉफ्ट कॉर्नर’ था। जब वो 60 साल के हुए तो उन्होंने उन्हें लिखा, ‘लोग आपसे शतायु होने के लिए कह रहे होंगे, मगर मैं आपसे ऐसा नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि आप जवान रहें और सक्रिय रहें।’
उनके बारे में परसाई ने लिखा था, ‘आँखों का उपयोग नामवरजी हथियार की तरह करते हैं। उनकी आँखों में शैतानी चमक तब भी आ जाती थी और आज भी आ जाती है। उनके लेखन में एक सहज प्रवाह है। उनकी भाषा में विलक्षण ‘तरलता’ है। कटाक्ष भी है और ‘वाकपटुता’ भी है।’
बेचन शर्मा उग्र से वाकयुद्ध
बेचन शर्मा उग्र एक फक्कड़ लीजेंड थे और बहुत ही बदज़बान भी। उनसे एक बार परसाई की चि_ी-पत्री हो गई। एक प्रकाशक ने उनसे एक कहानी संग्रह तैयार करने के लिए कहा।
उसमें उन्होंने उग्र की कहानी ‘उसकी माँ’ लेना तय किया। उग्र को लिख भी दिया कि प्रकाशक आपको 100 रुपए भेजेगा। पर प्रकाशक ने संग्रह छापने का विचार छोड़ दिया।
करीब पाँच महीने बाद परसाई को उग्र का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, वो पुस्तक तो अब खूब बिक रही होगी। प्रकाशक और तुम खूब पैसे कमा रहे होगे पर तुमने मुझे 100 रुपए नहीं भेजे। मैं तुम जैसे कमीने, बेईमान और लुच्चे लेखकों को अच्छी तरह से जानता हूँ।
परसाई ने उन्हें जवाब में लिखा, ‘प्रकाशक ने वो पुस्तक नहीं छापी, इसलिए आपको पैसे नहीं भेजे गए। जहाँ तक मुझे दी गई आपकी गालियों का सवाल है, मैंने काफी गालियाँ आप से ही सीखी हैं। और अपनी प्रतिभा से कुछ और गालियाँ जोड़ कर मैंने उनका काफ़ी बड़ा भंडार कर लिया है। मैं आपसे श्रेष्ठ गालियों का नमूना इसी पत्र में पेश कर सकता हूँ पर इस बार आपको छोड़ रहा हूँ।’
इसके जवाब में उनका एक कार्ड आया जिस पर सिर्फ इतना लिखा था ‘शाबाश प_े!’ (bbc.com/hindi)
-जेके कर
29 अगस्त को जारी हुरून इंडिया की देश के अमीरों की सूची-24 की माने तो देश के आधे सकल घरेलू उत्पादन पर केवल 1539 लोगों का कब्जा है जो पिछले साल से 220 ज्यादा है। इन खरबपतियों के 70 फीसदी के पास तो देश के सकल घरेलू उत्पादन का एक तिहाई से भी ज्यादा संपत्ति है।
इनके पास 1.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर के बराबर की कुल संपत्ति है। बकौल हुरून इंडिया इन लोगों की संख्या में पिछले सालों की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। इस सूची में नये 18 लोगों के पास 1 लाख करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की संपत्ति है जो पिछले साल से 6 ज्यादा है। एक दशक पहले मात्र 2 लोगों के पास 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हुआ करती थी। जाहिर है कि अमीर और अमीर हुये हैं। इससे जुड़ा हुआ लाख टके का सवाल है कि जब संपत्ति पर कब्जा सिमटता जा रहा है तो गरीबों का क्या हाल हुआ है, उस पर हुरून की सूची खामोश है। हुरून की सूची देश के अर्थव्यवस्था के हालत को बयां करती है कि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था चंद मुठ्ठियों में सिमटती जा रही है।
इसे अर्थशास्त्र के एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिये कि एक घर में 100 लोग रहते हैं तथा वहां पर 10 लाख की संपत्ति है। जिसमें से 5 लाख रुपये 1 व्यक्ति के पास है तो बाकी के बचे 99 लोगों में बचे हुये 5 लाख ही आयेगी अर्थात 5050 रुपये प्रति व्यक्ति। गौरतलब है कि हुरून हर साल देश तथा दुनिया के खरबपतियों की सूची जारी करती है। मीडिया में इस सूची के जारी होने के बाद जोरदार रिपोर्टिंग होती है लेकिन गरीबो तथा मध्यमवर्ग की कोई सुध नहीं लेता है। जब संपदा चंद मुठ्ठियों में सिमटकर रह गई है तो क्रयशक्ति भी निश्चित तौर पर इन्हीं की मुठ्ठियों में सिमटकर रह गई है जाहिर है कि जब आवाम के बहुसंख्य लोगों की खरीदने की क्षमता घटी है तो बाजार में मंदी आयेगी ही आयेगी। इसी कारण से लोग 5 रुपये में मिलने वाले पारले जी बिस्कुट तक खरीदने से पहरेज कर रहें हैं।
इस सूची के अनुसार गौतम अदाणी तथा परिवार 11।6 लाख करोड़ रुपयों की संपत्ति के साथ देश में पहले स्थान पर है। इनकी संपत्ति में 95 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी हैं। भारत में हर 5वें दिन एक अरबपति/ खरबपति बने हैं। इस तरह से 272 लोग अमीर हुये हैं जबकि देश की जनसंख्या 140 करोड़ के करीब की है। याने इतने लोग और गरीब हुये हैं।
बालीवुड के किंग शाहरूख खान 7,300 करोड़ रुपयों के साथ इस सूची में शामिल हैं। दूसरे नंबर पर जूही चावला परिवार आता है। इसके अलावा रितिक रोशन, करन जौहर तथा अमिताभ बच्चन का नाम भी इस सूची में बालीवुड की सूची में शामिल है।
हुरून इंडिया के प्रमुख अनास रहमान जुनैद का कहना है कि देश का बिजनेस फ्रेंडली वातावरण जिसके तहत 42 व्यापार समझौते हुये हैं तथा नये मैनुफैक्चरिंग ईकाईयों को कॉर्पोरेट टैक्स में 15 फीसदी की छूट दी गई है जिससे इस क्षेत्र में बढ़ौती हुई है।
हुरून इंडिया की साल 24 की सूची के अनुसार गौतम अदाणी परिवार के पास 11,61,800 करोड़ रुपये की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी परिवार के पास 10,14,700 करोड़ रुपयों की संपत्ति है। तीसरे नंबर पर हैं शिव नादर परिवार उनके पास 3,14,000 करोड़ की संपत्ति है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसारअंबानी ने हाल ही में अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। उस भव्यता को सारे देश को दिखाया गया। लेकिन क्या किसी टीवी ने ऐसी कोई खबर दिखाई है कि बेटी को ब्याह देने के बाद एक मध्यमवर्ग कितने कर्ज में डूब जाता है।
ऐसे समय में सरकार को ऐसी योजनायें लाना चाहिये जिससे गरीब तथा मध्यम वर्ग के हाथ में पैसे आये तथा वे बाजार की ओर रुख करें। लेकिन इसका उल्टा किया जा रहा है। आवाम की क्रयशक्ति बढ़ाने के बजाये कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की जा रही है, विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिये उसकी राह को आसान किया जा रहा है, इनकम टैक्स में छूट दी जा रही है जाहिर है कि मलाईदार तबके को छूट देने से बाजार की मंदी दूर नहीं होने वाली। आखिरकार देश के गिने-चुने 2 से 10 फीसदी लोग कितने कार, कपड़े, अन्न, मकान, दवा तथा सेवा का उपभोग कर सकते हैं। रईस होने से रोटी सूखी के बजाये घी लगाकर खाई जा सकती है, उस पर सोने-चांदी का लेप लगाकर तो खाया नहीं जा सकता है।
कुलमिलाकर, मामला यह है कि आम जनता के पास कितना पैसा आता है उस पर सब कुछ निर्भर करता है। हां, इसके लिये नीतियां बनानी पड़ेंगी। हुरून की सूची तो हर साल जारी होगी तथा खरबपतियों का बखान करेंगी जबकि जरूरत है कि गरीबों के उत्थान के लिये कुछ किया जाये। आपको, हुरून की सूची के दूसरे पहलू को जानकर कैसा लगा?
महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवन में राजकोट किले में बनी छत्रपति शिवाजी की मूर्ति ढहने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी से माफ़ी मांगी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं इस घटना पर सिर झुका कर माफी मांगता हूं। हमारे लिए शिवाजी आराध्य देव हैं।
उन्होंने यह बयान शुक्रवार को राज्य के पालघर जि़ले में वधावन बंदरगाह परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान दिया।
मोदी ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल हमारे लिए एक महान व्यक्ति हैं, बल्कि वह हमारे आदर्श हैं। मैं उस मूर्ति के चरणों में झुक रहा हूं और अब उनसे माफी मांग रहा हूं।
राजकोट किले में लगी शिवाजी की 35 फ़ुट की मूर्ति 26 अगस्त को ढह गई थी। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा था कि वो इस घटना पर सौ बार माफी मांगने को तैयार हैं। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी इस घटना के लिए माफी मांग चुके हैं।
शिवाजी की इस प्रतिमा का अनावरण बीते साल प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना दिवस के दिन किया था।
इस मूर्ति को लगाने का उद्देश्य शिवाजी की मराठा नौसेना और समुद्री सीमाओं की रक्षा की उनकी कोशिशों के प्रति सम्मान दिखाना था।
मूर्ति के ढहने के बाद विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने सत्ताधारी बीजेपी-शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट)-एनसीपी (अजित पवार गुट) गठबंधन पर निशाना साधा है और माफ़ी की मांग की है।
मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने भी मांगी माफी
29 अगस्त को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगी थी।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वह शिवाजी महाराज के चरणों में सौ बार सिर रखने को तैयार हैं।
उन्होंने कहा था, शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं, हमारी पहचान हैं। इस मामले का राजनीतिकरण न करें। वे माफ़ी की मांग कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बार नहीं, बल्कि सौ बार छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में अपना सिर रखने के लिए तैयार हूं। मुझे इससे कम महसूस नहीं होगा क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं।
उन्होंने यह भी मांग की है कि विपक्ष को यह बताना चाहिए कि जल्द से जल्द छत्रपति शिवाजी की मज़बूत मूर्ति लगाने के लिए क्या किया जा सकता है।
इस संबंध में 29 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास 'वर्षा' पर एक अहम बैठक हुई। जिसमें तमाम अधिकारी और नौसेना अधिकारी भी मौजूद रहे।
छत्रपति शिवाजी की मूर्ति ढहने के मामले में 29 अगस्त को राज्य सरकार ने जांच के लिए नौसेना के नेतृत्व में एक संयुक्त समिति बनाई थी।
नौसेना ने बताया है कि इस समिति में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ-साथ नौसेना के अधिकारी और तकनीकी जानकार शामिल होंगे।
वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले में एक दूसरी समिति की भी घोषणा की है। ये समिति मूर्ति की जगह पर जल्द से जल्द एक और मूर्ति लगाने के लिए काम करेगी।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह चुके हैं कि मूर्ति तेज़ हवाओं के कारण गिरी थी।
बुधवार को इस मामले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मूर्ति गिरने पर माफी मांगी।
लातूर जिले में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों से माफी मांगता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं और ये घटना यह हम सभी के लिए झटका है कि उनकी प्रतिमा एक साल के भीतर ढह गई।
प्रतिमा के केवल आठ महीनों के भीतर ढह जाने के बाद, इसकी काम की गुणवत्ता और इसके अनावरण में जल्दबाजी को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है।
सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच इस मुद्दे पर खींचतान देखी गई।
मूर्ति को लेकर विवाद
मूर्ति ढहने के मामले में बुधवार को बीजेपी नेता नारायण राणे और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और इस वजह से तनाव भी पैदा हो गया।
बुधवार को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने इस किले का दौरा किया और वहां विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की।
आदित्य ठाकरे के साथ इस दौरान अंबादास दानवे, वैभव नाइक और एनसीपी (शरद पवार) नेता जयंत पाटिल और कई समर्थक थे।
इसके जवाब में नारायण राणे के समर्थकों ने भी नारेबाज़ी कर विरोध जताने की कोशिश की। उनके साथ नीलेश राणे भी वहीं थे। पुलिस की ओर से दोनों गुटों से बातचीत कर तनाव कम करने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली।
इस दौरान भ्रम की स्थिति से बचने और मध्यस्थता के जरिए रास्ता निकालने के लिए शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल भी नीलेश राणे के साथ चर्चा करते नजऱ आए।
बाद में पत्रकारों से बात करते हुए जयंत पाटिल ने कहा, केवल आठ महीने पहले बनाई गई मूर्ति गिर गई है। यह मूर्ति नहीं गिरी है, महाराष्ट्र का गौरव गिरा है।
जयंत पाटिल ने कहा, मुख्यमंत्री कहते हैं कि तेज़ हवा चल रही थी इसलिए मूर्ति गिरी। अगर ऐसा होता तो दो या तीन पेड़ गिर जाते, लेकिन केवल मूर्ति ही गिरी। इसका मतलब है कि मूर्ति का काम सही तरीके से नहीं हुआ था। मूर्ति का काम किसी कम एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को गया था। जिसे दो फु़ट की मूर्ति बनाने का अनुभव है उसे 35 फु़ट की मूर्ति का काम दिया गया।
सरकार का कहना है कि मूर्ति नौसेना ने बनाई है। सरकार हाथ नहीं जोड़ेगी। यह सरकार की जि़म्मेदारी है। नौसेना के लोगों ने वहां मूर्ति स्थापित की लेकिन मूर्तिकार को किसने खोजा? नौसेना को इसके बारे में किसने जानकारी दी? यह कैसे विकास है? मूर्ति का ठेका किसे, कैसे मिला, इन सभी बातों की जांच होनी चाहिए।
महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस
महाविकास अघाड़ी ने रविवार यानी एक सितंबर को मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास लगी शिवाजी की प्रतिमा के पास सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन की घोषणा की है।
एनसीपी (शरद पवार गुट) के प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस प्रदेश प्रमुख नाना पटोले की मौजूदगी में मातोश्री में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा, महाविकास अघाड़ी सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेगी और सितंबर एक को हूतात्मा चौक से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया तक मार्च करेगी।
उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की इस सफाई को भी ये कह कर खारिज कर दिया कि ये बेशर्मी की हद है।
उद्धव ठाकरे ने कहा, अब राजकोट घटना के विरोध में विपक्ष जो विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने जा रही है उसमें मोदी सरकार के दलाल और शिवद्रोही रास्ता रोक रहे हैं। हवा के झोंके से महाराज की मूर्ति गिरने का कारण बताना बेहद शर्मनाक है।
उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सत्ताधारी गठबंधन सरकार का भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है और प्रशासन में स्थिति खराब हो गई है।
विपक्ष हमलावर
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने विपक्ष पर इस मामले को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया था।
इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने कहा, इसमें राजनीति कहां है? शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान जब एक लडक़ी के साथ बलात्कार हुआ तो शिवाजी ने व्यक्ति के हाथ और पैर कटवा दिए थे। उन्होंने लोगों के सामने अपराध को लेकर इतना सख्त रुख अपनाया था, लेकिन आज भ्रष्टाचार हुआ है। वो भी शिवाजी की प्रतिमा बनाने के फ़ैसले में।
उन्होंने कहा, जहां-जहां प्रधानमंत्री खुद गए हैं, वहां-वहां प्रतिमा गिरी है। इससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार किस हद तक पहुंच गया है। इसलिए विपक्षी गठबंधन ने महाराष्ट्र के लोगों से अपील करने और यह विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है।
वहीं नाना पटोले ने कहा, प्रतिमा के उद्घाटन के मौके पर खुद नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद थे। लेकिन प्रतिमा लगाने के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की गई हैं। इसका उद्घाटन में तब तक नहीं जाना चाहिए था जब तक कि संस्कृति मंत्रालय ने प्रतिमा को प्रमाणित नहीं कर दिया था। लेकिन यह सब यह दिखाने के लिए किया गया कि वो कितने शिव प्रेमी हैं।
सत्ता पक्ष का पलटवार
महाविकास अघाड़ी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी सांसद नारायण राणे ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महाविकास अघाड़ी की कड़ी आलोचना की।
उन्होंने कहा, शिवाजी की मूर्ति गिरने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। बारिश के मौसम में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण प्रतिमा ढह गई। मैं और जनता चाहते हैं कि किसी पर आरोप लगाने की बजाय इस मूर्ति को बनाने वालों की जांच होनी चाहिए। यह मूर्ति क्यों गिरी इसकी वजह सामने आनी चाहिए।
नारायण राणे ने कहा, उन्होंने हमें शिवसेना का गद्दार कहकर हमारी आलोचना की है, जबकि उन्होंने खुद शिवसेना के बनने के बाद से छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदुत्व को अपनी कमाई का साधन बना लिया है।
हमने कम से कम छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति लगाई है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के खर्च पर अपने पिता की मूर्ति बनवाई इसलिए इस मामले पर बोलने का उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। (bbc.com/hindi)
-सलमान रावी
कोलकाता के आर।जी। कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं।
विरोध-प्रदर्शन, बंद और हिंसा की घटनाओं के बीच अब प्रदेश के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।
गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार और वरिष्ठ नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। राज्यपाल से ‘अनुरोध’ किया था कि वह पश्चिम बंगाल में ‘संवैधानिक मूल्यों की रक्षा‘ करें।
इससे पहले 27 अगस्त को राज्यपाल ने भी बयान जारी कर ‘पश्चिम बंग छात्र समाज’ के बुलाए गए ‘नबन्ना मार्च‘ (सचिवालय पर प्रदर्शन) के दौरान हुई हिंसा को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की थी।
अब भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल को जो ज्ञापन सौंपा है, उसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान का उल्लेख किया गया है, जो उन्होंने बुधवार को दिया था।
बनर्जी ने ये बयान तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में दिया था।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था, ‘पश्चिम बंगाल में आग लगाने की साजिश हो रही है। अगर पश्चिम बंगाल जलेगा तो असम, पूर्वोत्तर राज्य, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे।’
दबाव में हैं ममता बनर्जी?
ममता बनर्जी के बयान की बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आलोचना की, जिनमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन। बीरेन सिंह भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान की आलोचना भी हो रही है, जिसमें उन्होंने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को काम पर वापस लौटने की सलाह देते हुए कहा था कि सरकार उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनका ‘भविष्य खराब हो जाएगा।’
पश्चिम बंगाल की राजनीति पर नजर रखने वाले मानते हैं कि मुख्यमंत्री के बयानों से यह झलकने लगा है कि आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या की घटना के बाद आम लोगों में पनपे आक्रोश से ममता बनर्जी दबाव में हैं।
कुछ जानकार कहते हैं कि उन्हें इतने दबाव में पहली बार देखा जा रहा है। वहीं कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें लगता है कि वह इससे जल्द ही उबर जाएंगी।
राजनीतिक विश्लेषक प्रोसेनजीत बोस कहते हैं कि ये सही है कि ये पहली बार नहीं है, जब ममता बनर्जी को आंदोलन का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन वो मानते हैं कि इस बार वो दबाव में इसलिए दिख रही हैं क्योंकि आम लोगों के बीच उनके शासन चलाने के तरीके की आलोचना हो रही है।
प्रोसेनजीत बोस कहते हैं, ‘महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार का ये रिकॉर्ड नहीं रहा है कि उसने किसी पीडि़ता को इंसाफ दिलवाया हो या फिर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों को कभी कानूनी शिकंजे में जकड़ा हो।‘‘
बोस कहते हैं कि आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद आम लोगों और खास तौर पर आम महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा, जिसका तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं, राज्य सरकार या खुद ममता बनर्जी को अंदाजा नहीं था।’
उनका कहना है कि जिस तरह से कोलकाता पुलिस की भूमिका इस मामले को लेकर रही, जैसे एफआईआर दर्ज करने में देरी, पीडि़ता के माता-पिता को गलत जानकारी दिया जाना या फिर घटना में ‘सिविल वॉलंटियर’ का शामिल होना-ये सब लोगों के गुस्से को बढ़ाता रहा।
बीबीसी से बात करते हुए प्रोसेनजीत बोस ने कहा, ‘कई चीजें एक साथ हुईं। जैसे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अन्य वरिष्ठ प्रशासकों की भूमिका। फिर अभियुक्त संजय राय पुलिस का ही हिस्सा है, बतौर एक सिविल वॉलंटियर। फिर 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात में आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में विरोध कर रहे जूनियर डॉक्टरों पर जो भीड़ का हमला हुआ, उससे कोलकाता पुलिस की छवि तो खराब हुई ही साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार भी आम लोगों के सवालों के घेरे में आ गई।’
सिर्फ एक घटना ही इन प्रदर्शनों की ‘असली वजह’ नहीं
पीडि़ता के परिवार और जूनियर डॉक्टरों के आक्रोश के बावजूद आर।जी। कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष पर प्रशासनिक कार्रवाई ना करते हुए, उनको कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का प्रिंसिपल बना दिया गया।
वो भी तब जब उनके खिलाफ ‘प्रशासनिक अनियमितताओं‘ के आरोपों की लिखित शिकायत राज्य सरकार के पास मौजूद थी।
यही वजह है कि पश्चिम बंगाल सरकार के रुख को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणियां कीं। इससे लोगों के बीच राज्य सरकार और ममता बनर्जी को लेकर आक्रोश भडक़ गया।
ऐसा पहली बार भी हुआ है कि आम लोगों के साथ-साथ, अलग-अलग ही सही, सभी विपक्षी दल, जैसे कांग्रेस और वाम दलों ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ इस घटना के बाद मोर्चा संभाला।
राजनीतिक विश्लेषक दिवाकर रॉय का कहना है कि प्रशासन के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा फूट पड़ा, वह सिर्फ एक घटना की वजह से नहीं है बल्कि कई मुद्दे हैं, जिनको लेकर लोगों में आक्रोश पहले से ही पनप रहा था।
वो कहते हैं कि पार्टी के अंदर ही अभिषेक बनर्जी ने कई बार यह मुद्दा उठाया कि राज्य प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है।
उनका कहना था, प्रशासन जिस तरह से चल रहा है, उसको लेकर भी लोगों में पहले से ही गुस्सा था। जैसे जन प्रतिनिधियों की थाना प्रभारियों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के सामने कुछ चलती ही नहीं थी।
वैसे देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में लोगों का राजनीतिक दलों पर से ही भरोसा कम होता जा रहा है। क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं की भाषा अगर आप सुनें तो एक तरह से उकसाने वाली भाषा बोलते हैं।
पहले ये आरोप वाम दलों पर लगते थे मगर अब तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं पर भी इसी तरह के आरोप लग रहे हैं। इसलिए वो गुस्सा आम लोगों में पनप तो रहा था, लेकिन आर।जी। कर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद लोगों के सब्र का बांध टूट गया।’
ममता बनर्जी की छवि पर असर
वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक मानते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है, जब आम लोगों के बीच ममता बनर्जी की छवि खराब हुई है। वह भी इसीलिए कि कोलकाता पुलिस और अस्पताल के प्रशासन पर फौरन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
लेकिन वो मानते हैं, ‘ममता दबाव में जरूर दिख रही हैं, मगर इससे उबरने की पूरी कोशिश कर रही हैं। उनके पास अब भी कई दांव मौजूद हैं। उन्होंने बलात्कार के अभियुक्तों को फांसी देने के लिए कानून लाने की बात भी कही है और भी बहुत कुछ है, उनके झोले में। तो यह कहना ठीक नहीं होगा कि उनका खेला खत्म हो रहा है। खेला खत्म नहीं हुआ है, जबकि भाजपा ने लोगों के इस आक्रोश को भुनाने की पूरी कोशिश की है।’
जानकार कहते हैं कि जिस तरह का दबाव ममता बनर्जी पर पिछले एक-दो दिनों में बन गया है, उससे बाहर निकलने के लिए वह आक्रामक तेवर भी दिखा रही हैं।
जिस तरह राज्य सरकार ने भारत बंद के दौरान गिरफ्तारियां की हैं या फिर ‘पश्चिम बंग छात्र समाज‘ के ‘नबन्ना मार्च‘ (सचिवालय मार्च) करने वालों पर क़ानूनी कार्रवाई की है, उससे वह फिर से चीजों को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है।
तृणमूल कांग्रेस के नेता मानते हैं कि ‘जिस तरह की राजनीति विपक्ष और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है,‘ उसको लेकर ममता बनर्जी का आक्रामक रवैया ही सही है।
तृणमूल कांग्रेस के नेता जय प्रकाश मजूमदार कहते हैं, हाल ही में लोकसभा के चुनावों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए हर हथकंडा अपनाया था, मगर जनता ने उन्हें नकार दिया।
मजूमदार कहते हैं, अब आर।जी। कर की घटना को लेकर बीजेपी अपनी राजनीति फिर से चमकाने की कोशिश कर रही है और राज्य में हिंसा और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है।
उनका कहना है कि राज्य सरकार ने घटना के फौरन बाद कार्रवाई की और एक अभियुक्त को कुछ ही घंटों में पकड़ लिया।
इसके बाद मामला सीबीआई के पास चला गया है, तो सवाल उन पर उठता है कि उन्होंने इतने दिनों में जांच में क्या प्रगति की है? यह इस घटना को लेकर राज्य को अशांत करने की साजिश कर रहे हैं, जिसका ममता बनर्जी ने भांडा फोड़ा है।’
मजूमदार का आरोप है कि केंद्र सरकार और खासतौर पर बीजेपी पश्चिम बंगाल को ‘राज्यपाल के जरिए अस्थिर करने की कोशिश‘ कर रही है। वह कहते हैं कि इससे पहले भी संदेशखाली को लेकर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी।
पश्चिम बंगाल बीजेपी के महासचिव जगन्नाथ चटर्जी इन आरोपों का खंडन करते हुए कहते हैं कि राज्यपाल अपना संवैधानिक धर्म निभा रहे हैं लेकिन उनके खि़लाफ़ भी साजि़श रची गई है।
वो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने ही पैदा किया है। उनका कहना था, ‘जैसे सामंतवादी व्यवस्था हुआ करती थी, ठीक उसी तरह से सरकार चलाई जा रही है। सभी कानून ताक पर रख दिए गए हैं।’
जगन्नाथ चटर्जी कहते हैं कि अब सिविल वॉलंटियर की भूमिका को ही ले लीजिए। ये कौन हैं। ये कैसे नियुक्त हुए? ये पुलिस के साथ बिना किसी प्रशिक्षण के कैसे काम कर रहे हैं। इन्हीं में से एक सिविल वॉलंटियर आर। जी, कर मेडिकल कॉलेज की घटना का अभियुक्त है। ये सब तृणमूल कांग्रेस के कैडर के हैं जो आम लोगों का दोहन करते हैं। हम सवाल उठा रहे हैं तो हम अराजक कैसे हुए ?’
वो कहते हैं कि सरकार ‘अपनी नाकामियों की वजह से घिर गई है।’
अब भी चल रहा है डॉक्टरों का प्रदर्शन
बुधवार की दोपहर का समय और कोलकाता के सबसे व्यस्ततम इलाके में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों का जुलूस खामोशी से आगे बढ़ता जा रहा है। ये सभी जूनियर डॉक्टर और नर्सिंग स्टूडेंट हैं। इनमें से कुछ आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज से हैं तो कुछ दूसरी मेडिकल संस्थाओं से।
‘वी वांट जस्टिस‘ या ‘हमें इंसाफ चाहिए लिखे’ हुए पोस्टर इनके हाथों में हैं और ये सब नौ अगस्त को हुई मेडिकल की छात्रा के बलात्कार और हत्या की घटना के ‘अभियुक्तों पर कार्रवाई की मांग’ कर रहे हैं।
नुक्कड़ नाटक के जरिए ये छात्र अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं।
आंदोलन डॉक्टरों का था जो अपनी सहकर्मी की हत्या और बलात्कार के दोषियों के लिए सजा की मांग कर रहे थे। मगर अब इन आंदोलनरत डॉक्टरों की आवाज राजनीतिक हिंसा और बयानबाजी के शोर में दबती जा रही है।
कोलकाता के श्याम बाजार के इलाके से विरोध मार्च निकाल रहे जूनियर डाक्टरों में से एक अनुपम कांति बाला कहते हैं कि अब मुख्य मुद्दा ही गौण होता जा रहा है।
बीबीसी से बात करते हुए उनका कहना था, हमारी सहपाठी के साथ बलात्कार हुआ फिर हत्या कर दी गई। कोलकाता पुलिस ने जांच की और अब सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन नतीजा क्या आया। नौ अगस्त की घटना है और अभी तक सिर्फ एक ही गिरफ्तारी हो पाई है।
अनुपम कांति कहते हैं कि कोलकाता पुलिस ने जिस तरह से मामले को लेकर रुख़ अपनाया था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से उसे फटकार मिल चुकी है। मगर अब सीबीआई क्या कर रही है? पता नहीं हमारी सहकर्मी को इंसाफ भी मिल पाएगा या नहीं। हमें आक्रोश से ज़्यादा दुख सता रहा है।’
प्रदर्शन में शामिल एक अन्य डॉक्टर, अनुपम रॉय कहते हैं, ‘अब हमारी मांगों की तरफ कोई नहीं देख रहा है। राजनीतिक दल आपस में कुश्ती कर रहे हैं। हमारा भविष्य, हमारी मांगें, पीडि़ता को इंसाफ या हमारी सुरक्षा- ये मुद्दे राजनीतिक दलों ने दबा दिए हैं।’ (bbc.com/hindi)
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को जमात-ए-इस्लामी पर लगी पाबंदी हटा ली है।
जमात-ए-इस्लामी के छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर और उसके अन्य संगठनों पर भी लगी पाबंदी हटा दी गई है।
इन संगठनों पर शेख़ हसीना सरकार के दौरान साल 2013 में पाबंदी लगाई गई थी। पिछले साल बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जमात के चुनाव लडऩे पर भी प्रतिबंध लगा दिया था।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गृह मंत्रालय ने 28 अगस्त को प्रतिबंध हटाने की अधिसूचना जारी की है।
जमात-ए-इस्लामी से पाबंदी हटा लेने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में उसके लिए विकल्प खुल गए हैं और देश के चुनावों में वह अपनी भूमिका निभा सकता है।
जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी है। इस पार्टी का छात्र संगठन काफ़ी मज़बूत है। इस पर देश में हिंसा और चरमपंथ को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं।
भारत में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पार्टी पर बांग्लादेश में हिन्दू विरोधी दंगे भडक़ाने का भी आरोप लगा था। जमात-ए-इस्लामी की छवि भारत विरोधी रही है।
साल 1990 में बांग्लादेश में सैन्य शासन ख़त्म होने के बाद जमात-ए-इस्लामी और इसके नेताओं पर युद्ध अपराध के आरोप लगे थे और उन पर मुक़दमा चला था।
साल 2010 में अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल ने पार्टी के आठ नेताओं को युद्ध अपराध का दोषी भी पाया था।
जमात ने पहली बार साल 1978 के चुनावों में हिस्सा लिया था। साल 2001 में बेग़म ख़ालिदा जिया के नेतृत्व वाली सरकार में यह पार्टी भी शामिल हुई थी।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, ‘जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश, इसकी छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिबिर और संगठन की अन्य सभी सहयोगी इकाइयों का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं मिला है।’
‘इसलिए सरकार का मानना है कि जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश, इस्लामी छात्र शिबिर और जमात की अन्य सभी सहयोगी इकाइयां आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं हैं।’
जमात प्रमुख ने भारत पर क्या कहा?
समाचार एजेंसी पीटीआई से जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफ़ीक़-उर रहमान ने कहा है कि भारत ने अतीत में कुछ ऐसे काम किए हैं जो बांग्लादेश के लोगों को पसंद नहीं आया है।
उन्होंने कहा, ‘मसलन साल 2014 के बांग्लादेश में चुनाव के दौरान एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक ने ढाका का दौरा किया और निर्देश दिया कि चुनावों में किसे भाग लेना चाहिए और किसे नहीं। यह अस्वीकार्य था, क्योंकि यह पड़ोसी देश की भूमिका नहीं है।’
जमात प्रमुख ने कहा, ‘हमारा मानना है कि भारत अंतत: बांग्लादेश के साथ संबंध में अपनी विदेश नीति का पुनर्मूल्यांकन करेगा। हमें लगता है कि एक-दूसरे के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए।’
उन्होंने कहा, ‘मिलकर काम करना और हस्तक्षेप करना दो अलग-अलग बात है। साथ मिलकर काम करना सकारात्मक मायने रखता है जबकि हस्तक्षेप नकारात्मक है। भारत हमारा सबसे कऱीबी पड़ोसी है। हम ज़मीन और समुद्री दोनों सीमाएं साझा करते हैं, इसलिए हमारे बीच अच्छे संबंध होने चाहिए।’
उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी भारत के साथ सौहार्दपूर्ण और स्थिर संबंध चाहती है, लेकिन साथ ही उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत को पड़ोस में अपनी विदेश नीति पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है, द्विपक्षीय संबंधों का मतलब एक-दूसरे के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप करना नहीं है। शफ़ीक़-उर रहमान ने बांग्लादेश में हाल ही में आई बाढ़ के हालात और भारत की भूमिका पर भी टिप्पणी की है।
हिन्दुओं पर हमलों के आरोपों को बताया बेबुनियाद
जमात-ए-इस्लामी पर शेख़ हसीना सरकार ने पाबंदी लगाई थी। लेकिन शेख़ हसीना के इसी महीने पाँच अगस्त को देश छोडक़र जाने के बाद से ही ढाका में जमात का दफ़्तर सक्रिय हो चुका था।
जमात के प्रमुख का कहना है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना अशांति की वजह से इस्तीफ़ा देकर भारत भागने की जगह क़ानून का सामना करतीं तो बेहतर होता।
रहमान ने स्वीकार किया कि अतीत में जमात-ए-इस्लामी का भारतीय प्रतिष्ठानों के साथ संपर्क था लेकिन पिछले 16 साल में अवामी लीग के शासन के दौरान ये संपर्क कम हो गया।
उनका मानना है कि भारत के साथ प्रभावी संबंध फिर से स्थापित किए जा सकते हैं।
बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी कार्यकर्ताओं के हिन्दुओं पर हमले के आरोपों को रहमान ने बेबुनियाद बताया है।
उन्होंने जमात-ए-इस्लामी के नकारात्मक चित्रण के लिए दुर्भावनापूर्ण मीडिया अभियान को जि़म्मेदार ठहराया है और कहा है, ‘पिछले 15 साल में शेख़ हसीना सरकार के अत्याचारों का सबसे ज़्यादा शिकार होने के बावजूद हम अब भी बचे हुए हैं और जमात को अब भी लोगों का समर्थन हासिल है।’
पाकिस्तान के साथ रिश्तों के बारे में रहमान ने कहा, ‘हम उनके साथ भी अच्छे संबंध चाहते हैं। हम उपमहाद्वीप में अपने सभी पड़ोसियों के साथ समान और संतुलित संबंध चाहते हैं। स्थिरता बनाए रखने के लिए यह संतुलन बहुत ज़रूरी है।’
जमात-ए-इस्लामी भारत विरोधी नहीं
शफ़ीक़-उर रहमान ने कहा, ‘हम यह नहीं कह रहे हैं कि भारी बारिश के लिए भारत जि़म्मेदार है लेकिन भारत को पानी छोडऩे से पहले हमें सूचित करना चाहिए था ताकि हम स्थिति को बेहतर तरीक़े से संभाल सकें और लोगों की जान बचा सकें।’
‘हमारा मानना है कि यह बांध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और पानी को उसके प्राकृतिक रास्ते पर चलने देना चाहिए।’
उनकी यह टिप्पणी ढाका से आई उन रिपोर्टों के बीच आई है, जिनमें बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए भारत को जि़म्मेदार ठहराया गया है।
बांग्लादेश और उससे सटे भारत के कई इलाक़ों में बारिश और बाढ़ से कई लोगों की मौत हो गई है और कऱीब 30 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
इस बाढ़ से राजनीतिक बदलाव के बाद बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।
भारत ने हाल ही में बांग्लादेश में आई उन रिपोर्टों का खंडन किया है, जिनमें कहा गया है कि त्रिपुरा में गुमती नदी पर बांध के खुलने की वजह से बांग्लादेश के कुछ इलाक़ों में बाढ़ आई है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी भारत और बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ संबंधों का समर्थन करती है, लेकिन बांग्लादेश को अतीत का बोझ पीछे छोडक़र अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मज़बूत और संतुलित संबंध बनाए रखना चाहिए।
रहमान ने तर्क दिया है कि जमात-ए-इस्लामी को भारत विरोधी मानने की भारत की धारणा ग़लत है और जमात-ए-इस्लामी किसी देश के ख़िलाफ़ नहीं है।
क्या है जमात-ए-इस्लामी संगठन
जमात-ए-इस्लामी की मूल शाखा जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश की स्थापना 26 अगस्त 1941 को लाहौर में हुई थी।
यह अविभाजित पाकिस्तान का समर्थक था। उसने साल 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद भी इसके लिए अभियान चलाया था।
डॉ. रहमान ने ढाका में पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि पाकिस्तान के शासन के दौरान हमारा बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन हमारे साथ भेदभाव किया जाता था।
डॉ. रहमान ने स्वीकार किया है कि बांग्लादेश कई धर्मों को मानने वाला देश है।
‘बांग्लादेश मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और अन्य छोटे धार्मिक समूहों से बना है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम सभी मिलकर बांग्लादेश बनाते हैं।’ (बाकी पेज 8 पर)
इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख़ हसीना और उनकी सरकार में मंत्री रहे सभी लोगों के राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं।
शफ़ीक़-उर रहमान ने कहा कि जब भी बांग्लादेश में चुनाव होंगे जमात-ए-इस्लामी उनमें भाग लेगी।
उन्होंने कहा, ‘हमारा मानना है कि अंतरिम सरकार को समय दिया जाना चाहिए, लेकिन यह अनिश्चितकालीन नहीं होना चाहिए। हम नए चुनावों के समय पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। लेकिन जब भी चुनाव होंगे, हम उसमें भाग लेंगे।’
1978 में जमात ने पहली बार आम चुनाव में हिस्सा लिया। 1986 में देश की संसद में उसके दस उम्मीदवार विजयी रहे।
साल 2001 में पार्टी ने संसद में 18 सीटें हासिल कीं और तीन अन्य दलों के साथ गठबंधन बनाया
इसी साल पार्टी बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार में शामिल हुई।
जमात पर लगे अहम आरोप
1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पार्टी के कई नेताओं पर लोगों पर अत्याचार के संगीन आरोप लगे।
पार्टी पृथक बांग्लादेश का विरोध कर रही थी क्योंकि उसकी निगाह में ये इस्लाम विरोधी था
1990 में सैन्य शासन के समाप्त होने के बाद पार्टी और उसके नेताओं के ख़िलाफ़ युद्ध अपराध में शामिल होने के आरोप लगे और मुक़दमे चले
मई 2008 में बांग्लादेश पुलिस ने जमात नेता और पूर्व मंत्री मतीउर रहमान को दो अन्य पूर्व मंत्रियों के साथ गिरफ्तार किया
गिरफ़्तार किए गए दो अन्य पूर्व मंत्री थे- अब्दुल मन्नान भुइयां और शम्सुल इस्लाम
साल 2010 में अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल ने पार्टी के आठ नेताओं को युद्ध अपराध का दोषी पाया
भारत में बाबरी विध्वंस के बाद पार्टी के नेताओं और छात्र संगठन पर बांग्लादेश में हिन्दू विरोधी दंगे भडक़ाने का भी आरोप है। (bbc.com/hindi)
-अशोक पांडे
1906 की अपनी अमेरिका-यात्रा के बाद मैक्सिम गोर्की ने तत्कालीन अमेरिकी समाज को लेकर कुछ बेहद तीखे लेख लिखे थे जो ‘पीले दैत्य का नगर’ शीर्षक किताब के रूप में छपे। पैसे की अंधी दौड़ में हर मानवीय मूल्य को अपनी सुविधा के हिसाब से तोड़-मरोड़ कर आम जन को बरगलाने का जो खेल उस समय खेला जा रहा था उसकी स्पष्ट प्रतिछाया आज हमारे समाज में दिखाई देती है।
इस बेहद जरूरी किताब के एक लेख में गोर्की का सामना एक ऐसे शातिर शख्स से होता है जो खुद को नैतिकता का पुरोहित बताता है। वह एक ऐसी संस्था द्वारा दिहाड़ी पर रखे गए असंख्य गुर्गों में से एक है जिसका इकलौता काम नैतिकता की आम समझ को ऐसी दिशा में मोडऩा है जहाँ वह केवल रईसों और सत्ताधारियों के पहले से सुविधासंपन्न जीवन अधिक आसान बना सके। उस छद्म नैतिकता में उनके द्वारा किये जाने वाले सारे पाप बगैर किसी हलचल के जज़्ब हो जाते हैं।
संस्था कैसे काम करती है इस बारे में वह कुछ दिलचस्प बातें बताता है, ‘नैतिकता के बारे में लगातार एक कोलाहल चलता रहना चाहिए ताकि जनता के कान बहरे होते रहें और उसे कभी सच सुनने को न मिले। अगर आप नदी में ढेर सारे कंकड़ फेंकें तो उनकी बगल से एक बड़ा लठ्ठा बिना लोगों की निगाह में आए निकल सकता है। या अगर आप बिना बहुत सावधानी बरते अपने पड़ोसी की जेब से उसका बटुआ निकालते हैं, लेकिन तुरंत ही फुटपाथ पर मुठ्ठीभर चने चुराकर भाग रहे बच्चे की तरफ लोगों का ध्यान बंटा देते हैं तो आप बच जाएँगे। बस आपको अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना है- ‘पकड़ो-पकड़ो’। हमारी संस्था बहुत सारी छोटी-छोटी वारदातें करता है ताकि बड़े पापों पर किसी की निगाह न जा सके।’
‘मिसाल के लिए शहर में अफवाह उडऩे लगती है कि एक सम्मानित नागरिक अपनी बीवी को पीटता है। संस्था तुरंत मुझे और बाकी कर्मचारियों को आदेश देती है कि हम अपनी बीवियों को पीटें। हम तुरंत वैसा ही करते हैं। बीवियों को यह पता ही होता है, पर वे अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती हैं। सारे अखबार इस बारे में लिखते हैं और इससे उपजने वाले कोलाहल में सम्मानित नागरिक के बारे में उड़ रही अफवाहें थम जाती हैं। अफवाह पर कौन ध्यान दे, जब आपके सामने ठोस तथ्य मौजूद है?’
‘हो सकता है कि अफवाहें उडऩे लगें कि सीनेट के सदस्य रिश्वत लेते हैं। संस्था तुरंत कई सारे पुलिस अधिकारियों द्वारा रिश्वत लिए जाने की घटनाओं को जनता के सामने रख देती है। एक बार फिर तथ्यों के सामने अफवाहें डूब जाती हैं। ऊँची सोसाइटी में कोई साहब किसी महिला का अपमान कर देते हैं। इस बात की तुरंत व्यवस्था कर दी जाती है कि होटलों और सडक़ों पर कई सारी महिलाओं का अपमान किया जाए। ऊँची सोसाइटी वाले साहब का अपराध इस तरह के अपराधों की श्रृंखला में खो जाता है।’
‘संस्था उच्च-वर्ग को जनता के फैसले से बचाकर रखती है। साथ ही नैतिकता के विरुद्ध हो रहे अपराधों को लेकर एक सतत कोलाहल बनाया जाता है ताकि लोगों को छोटी वारदातों के अलावा कुछ और के बारे में सोचने का अवसर न मिले और अमीरों के पाप छिपे रहें।’
-जोआ ओ द सिल्वा
ऑस्ट्रेलिया में ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ का एक नया नियम लागू हो गया है, जिसमें उन लोगों को राहत दी गई है जो दफ्तर में काम के बाद कंपनी के कॉल्स और मैसेज का जवाब देने के लिए मजबूर महसूस करते हैं।
नया क़ानून कर्मचारियों को ड्यूटी टाइम के बाद किसी भी संदेश को बिना बॉस के डर के नजऱअंदाज करने की आजादी देता है।
पिछले साल प्रकाशित एक सर्वे में यह बताया गया था कि ऑस्ट्रेलियाई लोग बिना किसी भुगतान के सालभर औसतन 280 घंटे ओवरटाइम करते हैं।
20 से ज़्यादा देशों में, खासतौर पर यूरोप और लैटिन अमेरिका में यह नियम लागू है।
इस क़ानून में नियोक्ताओं (एम्प्लॉयर्स) को ड्यूटी टाइम के बाद कर्मचारियों से संपर्क बनाने से नहीं रोका गया है।
इसकी बजाय, यह कर्मचारियों को तब तक जवाब नहीं देने का अधिकार देता है, जब तक उनके इनकार को अनुचित ना माना जाए।
इस क़ानून के अनुसार, नियोक्ताओं और कर्मचारियों को आपस के विवाद को खुद ही सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए।
दोनों विवाद को सुलझाने में असफल रहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का फ़ेयर वर्क कमिशन (एफड़ब्ल्यूसी) हस्तक्षेप कर सकता है।
एफड़ब्ल्यूसी नियोक्ता को ड्यूटी टाइम के बाद संपर्क बनाने से रोकने का आदेश दे सकता है।
अगर उसे लगता है कि किसी कर्मचारी का जवाब नहीं देना अनुचित है तो वह उन्हें जवाब देने का आदेश दे सकता है।
एफड़ब्ल्यूसी के आदेशों का पालन नहीं करने पर कर्मचारी पर 19,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर (कऱीब 10 लाख रुपये) और किसी कंपनी पर 94,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर (कऱीब 53 लाख रुपये) का ज़ुर्माना लगाया जा सकता है।
कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने इस क़ानून का स्वागत किया है।
ऑस्ट्रेलियाई ट्रेड यूनियन परिषद ने कहा, ‘यह कर्मचारियों को ड्यूटी टाइम के बाद अनुचित संपर्क से इंकार करने और बेहतर वर्क लाइफ को संतुलित करने में सक्षम और सशक्त बना।’
एक वर्क प्लेस विशेषज्ञ ने बीबीसी को बताया कि नए नियम नियोक्ताओं की भी मदद करेगा।
स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के जॉन हॉपकिंस ने कहा, ‘कोई भी संगठन जिसके कर्मचारी बेहतर आराम करते हैं और जिनकी वर्क लाइफ का संतुलन अच्छा है, उनके बीमार होने की संभावना कम होगी और कंपनी छोडऩे की भी संभावना कम होगी। इससे भी कर्मचारी को फायदा होगा और वह नियोक्ता के लिए भी फायदेमंद होगा।’
हालांकि, कर्मचारियों ने नए क़ानून पर मिलाजुली प्रतिक्रिया दी है।
विज्ञापन उद्योग में कार्यरत राचेल अब्देलनौर ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा, ‘मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि इस तरह के कानून हों।’
‘हम अपना बहुत सारा समय फोन पर बिताते हैं, पूरा दिन ईमेल से जुड़े रहते हैं और मुझे लगता है कि इसे बंद करना वाक़ई मुश्किल है।’
हालांकि, दूसरों को नहीं लगता कि नए नियमों से उन्हें कोई खास फर्क पड़ेगा।
वित्तीय उद्योग में कार्यरत डेविड ब्रेनन ने रॉयटर्स से कहा, ‘मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन आइडिया है। मुझे उम्मीद है कि यह लोगों को पसंद आएगा। हालांकि, सच कहूं तो मुझे संदेह है कि यह हमारी इंडस्ट्री में काम करेगा।’
उन्होंने कहा, ‘हमें अच्छा वेतन मिलता है, हमसे नतीजे की उम्मीद की जाती है और हमें लगता है कि दिन में 24 घंटे काम करना है।’(bbc.com/hindi)
पीएम नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे की चर्चा अब तक जारी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने 26 अगस्त को पीएम मोदी से जब फोन पर बात की, तो उनके यूक्रेन दौरे को लेकर भी चर्चा हुई।
भारत के विदेश मंत्रालय के जारी बयान के मुताबिक, पीएम मोदी ने बाइडन को यूक्रेन दौरे के बारे में जानकारी दी।
पीएम मोदी ने बातचीत और कूटनीति के ज़रिए समाधान तलाशने की अपनी नीति को दोहराया। उन्होंने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के जल्द लौटने को लेकर अपना पूरा समर्थन देने की बात कही।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने भी पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे, वहां मानवीय मदद पहुंचाने और शांति को लेकर भारत की कोशिशों की तारीफ की।
इससे पहले पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की चर्चा तब से सुनाई देने लगी थी, जब इस दौरे का एलान ही हुआ था।
पहले पीएम मोदी के यूक्रेन जाने की टाइमिंग और मकसद पर सवाल उठे। फिर पीएम मोदी जब यूक्रेन दौरे को खत्म करके भारत लौट ही रहे थे, उसी दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदीमीर जेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, उस पर भी जानकारों ने सवाल खड़े किए हैं।
पीएम मोदी के जाते ही जेलेंस्की का रुख़
पीएम मोदी जब यूक्रेन पहुंचे तो ज़ेलेंस्की से गले मिले और इस दौरान कुछ पल ऐसे भी रहे, जिसमें मोदी जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आए।
जुलाई में रूस दौरे पर गए मोदी जब पुतिन से गले मिले थे तो इसकी आलोचना करने वालों में ज़ेलेंस्की भी रहे थे।
ऐसे में मोदी का जेलेंस्की से गले मिलने को कुछ लोगों ने संतुलन बनाए रखने से जोडक़र देखा।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी यूक्रेन में हुई प्रेस वार्ता के दौरान एक पत्रकार के पूछे सवाल पर जवाब दिया, ‘दुनिया के जिस हिस्से में हम रहते हैं, वहां लोग मिलने पर एक-दूसरे को गले लगाते हैं। ये आपकी संस्कृति का हिस्सा नहीं होगा पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मैंने आज देखा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी गले लगाया।’
ज़ेलेंस्की को पीएम मोदी ने भले ही गले लगाया हो लेकिन जैसे ही वो भारत की ओर निकले, जेलेंस्की के बयानों ने दूरियों की ओर इशारा किया।
जेलेंस्की ने आखिर कहा क्या था
ज़ेलेंस्की ने 23 अगस्त को भारतीय पत्रकारों से हुई प्रेस वार्ता में भारत को लेकर कई बातें कहीं। ये बातें भारत को असहज करने वाली थीं।
ज़ेलेंस्की ने कहा था, ‘मैंने पीएम मोदी से कहा कि हम भारत में वैश्विक शांति सम्मेलन रख सकते हैं। ये एक बड़ा देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन हम ऐसे देश में शांति सम्मेलन नहीं रख सकते जो पहले शांति सम्मेलन में जारी हुए साझा बयान में शामिल नहीं हुआ।’
स्विटजऱलैंड में यूक्रेन में शांति को लेकर सम्मेलन हुआ था। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी (पश्चिम) पवन कपूर शामिल हुए थे। इस सम्मेलन के बाद जारी हुए साझा बयान से भारत ने दूरी बनाई थी। भारत ने अपने जूनियर अधिकारी को भेजा था जबकि कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक गए थे।
इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने रूस से भारत के तेल खरीदने पर भी बात की थी। जेलेंस्की ने कहा था, ‘अगर भारत रूस से तेल ना खरीदे तो उसे बड़ी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना होगा।’
यूक्रेन-रूस युद्ध के दौरान भारत ने रूस के तेल खरीदना जारी रखा था। ये खरीद ऐतिहासिक थी और तेल सस्ता होने के कारण भारत को इससे फायदा भी हुआ।
चीन-भारत के संदर्भ में पूछे सवालों के जवाब में ज़ेलेंस्की ने कहा था, ‘अगर पुतिन की हरकतों को जायज़ ठहराया जा सकता है तो मुझे यकीन है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इसके अंजाम सीमा नियमों के उल्लंघन के तौर पर देखने को मिलेंगे।’
पुतिन के बारे में जेलेंस्की ने कहा, ‘वो हमारे लिए हत्यारा है। लेकिन मोदी के रूस दौरे के दौरान जब बच्चों के अस्पताल पर हमला किया तो क्या पुतिन ने आपके लिए कुछ अच्छा किया? ये बहुत अहम पल था। पुतिन भारत का सम्मान नहीं करते।’
जेलेंस्की ने कहा था, ‘अगर भारत रूस के लिए अपना रुख़ बदल दे तो युद्ध रुक जाएगा। कई देशों ने रूस से आयात बंद कर दिया है पर भारत ने नहीं किया है। हमें रूसी सेना को ताकतवर बनाने वाले रुपयों को देना बंद करना होगा।’
संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने यूक्रेन में युद्ध को लेकर रूस के खिलाफ लाए गए कई प्रस्तावों से दूरी को बनाए रखा। वैश्विक मंचों पर भारत ऐसी किसी कोशिश में शामिल नहीं दिखा, जहां बात रूस के खिलाफ की जा रही हो।
जेलेंस्की ने कहा, ‘हम इस बात से ख़ुश नहीं हैं कि हमें भारत का साथ नहीं मिला। अब हमें प्रस्तावों से पहले बात करनी होगी। हमारे पास अतीत में जाने का वक़्त नहीं है। मैं कुछ अच्छा और सकारात्मक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भारत हमारी तरफ रहे।’
जेलेंस्की के रुख पर जानकारों ने उठाए सवाल
यूक्रेन के राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया की आलोचना पहले भी होती रही है। जेलेंस्की कई बार अमेरिका और ब्रिटेन को भी सैन्य मदद के मामले में देरी को लेकर आड़े हाथों लेने से बाज नहीं आए हैं।
जेलेंस्की से पिछले साल जुलाई में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री और अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार ने कहा था कि यूक्रेन को थोड़ी कृतज्ञता दिखानी चाहिए।
ज़ेलेंस्की से ब्रिटेन के तत्कालीन रक्षा मंत्री बेन वालैस ने कहा था, ‘हम इसे पसंद करें या ना करें लेकिन लोग चाहते हैं कि थोड़ी और कृतज्ञता होनी चाहिए। मैंने उनसे पिछली बार कहा था कि हम एमजॉन नहीं हैं कि आप मुझे लिस्ट थमा दें और हम डिलिवर कर दें।’
भारत के पूर्व विदेश सचिव और रूस में भारत के राजदूत रहे कंवल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर जेलेंस्की के बयानों पर प्रतिक्रिया दी।
अस्पताल पर रूसी हमले के संदर्भ में कंवल सिब्बल ने कहा, ‘जेलेंस्की की ऐसी अनुचित टिप्पणी गरिमापूर्ण नहीं है। ये कूटनीतिक कुशलता का अभाव है।’
सिब्बल ने लिखा, ‘मोदी के दौरे के बाद जेलेंस्की की टिप्पणी उचित नहीं थी। तेल खरीदने को लेकर भारत को खरी खोटी सुनाई गई, वो भी तब जब महीनों से भारत इस मामले पर अपना रुख बताता आया है। ऐसे में इसे दोबारा छेडऩे की क्या ज़रूरत थी? मोदी के दौरे में रूस के बम गिराने को अपमान से जोडऩा गंदी राजनीति है। भारत की ओर से शांति की कोशिशों और शांति समझौतों को लेकर जेलेंस्की ने जो कहा, वो भी सही नहीं था।’
सिब्बल ने कहा, ‘ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि भारत रूस-यूक्रेन के बीच संतुलन को छोडक़र यूक्रेन की तरफ आ जाए। ये परिपक्व राजनीति नहीं है। मोदी अच्छे इरादे के साथ यूक्रेन गए थे।’
पत्रकार करण थापर को दिए इंटरव्यू में कंवल सिब्बल ने कहा, ‘ज़ेलेंस्की ने जो कहा वो अनुचित, अपमानजनक और बेरुखी से भरा था। जेलेंस्की ने संदेश देने की कोशिश की है। इस मामले में जब अभी तक कोई अंतरराष्ट्रीय जांच नहीं हुई है तो ज़ेलेंस्की ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि मोदी जाकर पुतिन से कहेंगे कि तुम जिम्मेदार हो।’
थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन में इंडो पैसिफिक के विश्लेषक डेरेक जे ग्रॉसमैन ने पीएम मोदी के ज़ेलेंस्की को गले लगने वाली तस्वीर को साझा कर लिखा- ये बहुत बुरा है कि मोदी सबको गले लगाते हैं और इस कारण इसका कोई मतलब नहीं रह जाता।
ग्रॉसमैन ने बाइडन और मोदी की बातचीत के बाद जारी हुए बयान को साझा करते हुए लिखा- कोई फर्क नजर आया? अमेरिका के बयान में बांग्लादेश का जिक्र नहीं है।
हालांकि भारत की ओर से जारी बयान में लिखा है- बाइडन और मोदी के बीच बांग्लादेश के मुद्दे पर बात हुई।
भारत के पूर्व राजनयिक और अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार एमके भद्रकुमार ने रूस की वेबसाइट आरटी के लिए एक लेख लिखा है।
एमके भद्रकुमार लिखते हैं, ‘यूक्रेन के मुद्दे पर भारत के रुख को लेकर ज़ेलेंस्की का असंतोष बढ़ा दिखता है। भारत की नीति पर जैसी बातें कही गईं, उन पर गौर किया जाएगा। हालांकि रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध जारी रहेंगे।’
एमके भद्रकुमार ने कहा, ‘मोदी के ताज़ा दौरे से ये पता चलता है कि रूस से संबंध एक ऐसा क्षेत्र है, जहां अमेरिका और यूक्रेन को जाने की अनुमति नहीं है।’
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने कहा, ‘मोदी का यूक्रेन दौरा न सिर्फ गलत समय पर किया गया बल्कि इस दौरान जेलेंस्की ने मोदी की आलोचना की। उन्होंने न सिर्फ भारत की मध्यस्थता कराने की बात को खारिज किया बल्कि तेल खरीदने और संयुक्त राष्ट्र की वोटिंग में भारत के दूरी बरतने के मुद्दे पर भी घेरा।’
रूस यूक्रेन युद्ध और भारत
भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। पीएम मोदी जुलाई 2024 से पहले भी अतीत में रूस दौरे पर जा चुके हैं।
राजनयिक रिश्तों के करीब तीन दशकों में पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने यूक्रेन का दौरा किया है।
फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस ने आक्रमण किया था। तब से युद्ध जारी है।
हाल ही में रूस के अंदर यूक्रेनी सेना घुसी है और कुछ जगहों पर नियंत्रण पा लिया है।
इस युद्ध में अमेरिका समेत पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं और रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं।
इस मामले में भारत संतुलन बनाए रखने की नीति अपनाता रहा है। भारत ने प्रतिबंधों के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा था। हालांकि इस पर पश्चिमी देशों की नाराजगी भी देखने को मिली थी, मगर भारत ने अपना रुख नहीं बदला था। इस बीच भारत यूक्रेन को भी मानवीय मदद भिजवाता रहा है।
भारत के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक़, 2021-22 वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच 3।3 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था।
वहीं रूस और भारत के बीच करीब 50 अरब डॉलर से ज़्यादा का व्यापार हुआ। दोनों देशों के बीच आने वाले समय में कारोबार 100 बिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।
युद्ध के मामले में जब संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता तो भारत उससे दूरी बरतता दिखता।
हालांकि पीएम मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है। पीएम मोदी ने ये बात 2022 में पुतिन से भी कही थी।
-अशोक पांडे
करीब ढाई सौ बरस पहले आगरे के ताजगंज में रहने वाले दिग्गज शायर नज़ीर अकबराबादी ने कृष्ण के जन्म का वर्णन यूं किया है –
फिर आया वां एक वक़्त ऐसा जो आये गरभ में मनमोहन
गोपाल, मनोहर, मुरलीधर, श्रीकिशन, किशोरन कंवल नयन
घनश्याम, मुरारी, बनवारी, गिरधारी, सुन्दर स्याम बरन
प्रभुनाथ, बिहारी, कान्ह लला, सुखदाई जग के दुःख भंजन
जब साअत परगट होने की, वां आई मुकुट धरैया की
अब आगे बात जनम की है, जै बोलो किशन कन्हैया की
था नेक महीना भादों का, और दिन बुध, गिनती आठन की
फिर आधी रात हुई जिस दम और हुआ नछत्तर रोहिनी भी
सुभ साअत नेक महूरत से, वां जनमे आकर किशन जभी
उस मन्दिर की अंधियारी में, जो और उजाली आन भरी
नज़ीर के यहाँ कृष्ण भक्ति के मीठे रस की सदानीरा बहती है. एक नज़्म में वे श्रीकृष्ण से यूं मुखातिब होते हैं -
कहता नज़ीर तेरे जो दासों का दास है
दिन रात उसको तेरे ही चरनों की आस है
यूं उनके रचनाकर्म में गणेश जी भी आते हैं और भैरों भी, गुरु नानक जी भी और हरि भी, लेकिन कृष्ण के प्रति उनका अनुराग किसी स्फटिक की ठोस पारदर्शी चमक जैसा जादुई है. नज़ीर अकबराबादी के काव्य में कृष्ण का जीवनवृत्त कितने ही विवरणों और रूप-सरूपों में नज़र आता है और वे घोषणा करते हैं -
दिलदार गवालों बालों का, और सारे दुनियादारों का
सूरत में नबी, सीरत में खुदा या सल्ले अला
अल्लाहो ग़नी, अल्लाहो ग़नी
हे कृष्ण कन्हैया नन्द लला, अल्लाहो ग़नी, अल्लाहो ग़नी
भक्ति से सराबोर उनके काव्य का जो हिस्सा कृष्ण की बाल-लीलाओं को समर्पित है, उसकी ज़ुबान का संगीत और निश्छल-निर्बाध पोयटिक प्रवाह मिल कर नज़ीर को हमारी पूरी सांकृतिक विरासत के एक बड़े प्रतिनिधि के तौर पर स्थापित करते हैं.
यूँ बालपन तो होता है हर तिफ़्ल का भला
पर उनके बालपन में तो कुछ और भेद था
इस भेद की भला जी, किसी को ख़बर है क्या
क्या जाने अपने खेलने आए थे क्या कला
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन
क्या-क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन
एक कविता उनके ब्याह को लेकर है, एक उनके बचपन के खेलों के बारे में. एक में नज़ीर बताते हैं कि नरसी मेहता के मन में कृष्ण की लगन कैसे उपजी तो एक में कृष्ण और सुदामा की विख्यात कथा का दिलचस्प बयान है.
हर जन्माष्टमी को मुझे बाबा नज़ीर की पुरानी किताब निकाल कर उनके कृष्ण-काव्य में डूब जाना होता है -
सब ब्रज बासिन के हिरदै में आनंद खुशी उस दम छाई
उस रोज़ उन्होंने ये भी नज़ीर इक लीला अपनी दिखलाई
ये लीला है उस नन्द ललन मन मोहन जसुमति छैया की
रख ध्यान सुनो दंडौत करो, जै बोलो किशन कन्हैया की
नज़ीर के कृष्ण हम सब के हैं!
- डॉ. आर.के. पालीवाल
आजकल सरकार और सरकारी उडऩखटौलों और रथों में बैठे मंत्री और उसमें बैठे अधिकांश बड़े नौकरशाहों ने मिलकर एक ऐसा संगठित गिरोह सा बना लिया है जिसके आसपास जाना तो दूर अपनी समस्या या व्यथा पहुंचाना आम आदमी के लिए असंभव है। जब शासन के ऊंचे शिखरों तक जनता की पहुंच ही नहीं है तब उसके छोटे-छोटे काम संपन्न कराने के लिए दलालों का भ्रष्टाचार पथ ही एकमात्र विकल्प बचता है। पंचायत में बैठे पटवारी,थाने, पुलिस चौकी से लेकर हर विभाग के निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी जानते हैं कि उनके जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से लेकर चीफ सेक्रेटरी और डी जी पुलिस तक के उच्च अधिकारियों का अधिकांश वक्त राजनीतिक आकाओं की इच्छापूर्ति और जी हुजूरी में ही बीतता है, इसीलिए उन्हें ऊपर शिकायत होने का कोई डर नहीं है।
इधर निम्न श्रेणी के बहुतेरे अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी अपने इलाके के मंत्री, सांसद और विधायक का संरक्षण हासिल कर लिया जिससे न किसी की शिकायत पर उनका तबादला हो सकता और न उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही संभव है। इसी सब के चलते जो बेहद असंवेदनशील वातावरण तैयार हुआ है उसी ने सरकार और शासन को अंधे बहरे की नकारात्मक उपाधि दी है।
शासन के उच्च अधिकारियों का व्यवहार भी नेताओं की अत्यधिक संगत में रहकर एक तरफा हो गया। वे भी जूनियर अधिकारियों की बैठक लेते वक्त केवल और केवल बोलते हैं नीचे वालों की फीडबैक और परेशानियां नहीं सुनते। बोलने के लिए शासन के शिखर पर सवार मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के कई कई मुंह हैं, मसलन उनका एक मुंह वह है जिससे वे कहीं न कहीं भाषण देते रहते हैं या अपने मातहदों को आदेश देते हैं, एक मुंह ट्विटर (जिसका नया नाम एक्स हो गया) है जिस पर वे घड़ी घड़ी विकास की फुलझड़ी छोड़ते रहते हैं, एक मुंह फेसबुक अकाउंट और विभागीय वेबसाइट है और एक मुंह मीडिया को जारी किए जाने वाले विज्ञापन हैं जिनमें जमकर बड़े बड़े झूठ आकर्षक बनाकर परोसे जाते हैं।आप इन्हें किसी भी वक्त फोन कीजिए, इनके व्हाट्स ऐप नंबर पर मैसेज कीजिए , मेल भेजिए या चि_ी लिखिए या बारी बारी संवाद के यह सब साधन अपनाकर देख लीजिए वे आपके पत्र, मेल या मैसेज पर कोई संतोषजनक कार्यवाही तो दूर उसकी प्राप्ति की स्वीकृति तक नहीं देते।
मंत्रियों और उच्च अधिकारियों का फील्ड में उतरकर जनता की समस्याओं का देखना तो पूरी तरह बंद ही हो गया। जिन मंत्रियों को जिले की जिम्मेदारी दी जाती है वे जब तब सरकारी दौरे पर आते हैं और सर्किट हाउस के बंद कमरों में अपने चेले चपाटों से मिलकर कब निकल जाते हैं इसका पता अगले दिन के अखबार से मिलता है। मुख्यमंत्री और मंत्री राजधानी के बाहर निकलते हैं तो अपने परिचितों और रिश्तेदारों के निजी कार्यक्रमों में ज्यादा समय देते हैं जनता की समस्याओं पर नहीं के बराबर। लोकतंत्र विकृत होते होते राजशाही की तरह दो ध्रुवीय हो गया। जन प्रतिनिधि राजा और वजीर बन गए और प्रजा गुलाम बन गई। नौकरशाही का काम राजा और उनके वजीरों की बादशाहत बरकरार रखना और प्रजा को डरा धमकाकर भेड़ बकरी की तरह आज्ञाकारी बनाना हो गया।
आजादी के अठहत्तर साल से केवल दो बार आधी अधूरी बदलाव की लहर उठी है लेकिन दोनों बार यह लहर ज्वार में नहीं बदल पाई। आपातकाल के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में तत्कालीन केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हुआ था।
इस अहिंसक आंदोलन के पीछे जय प्रकाश नारायण के विराट व्यक्तित्व और जनता में उनके प्रति विश्वास का भाव था क्योंकि उन्होने न केवल आजादी के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी अपितु विनोबा भावे के साथ मिलकर गांधी की सर्वोदय सेवा परंपरा को आगे बढ़ाया था। दूसरा छोटा आंदोलन अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुआ था लेकिन वह दिल्ली तक सीमित रहा। उम्मीद की जानी चाहिए कि निकट भविष्य में कोई बड़ा जन आंदोलन हो जिससे अंधी बहरी सरकारों का अंधा और बहरापन हमेशा के लिए दूर हो।
-श्रवण गर्ग
पत्रकार-मित्र सुनील कुमार ने फ़ेसबुक पर डिजिटली-निर्मित अथवा रंगों से उकेरा गया एक चित्र शेयर किया था। चित्र में ‘मोनालिसा’ जैसी दिखने वाली एक महिला आकृति को किसी पुरुष से प्रेम करते हुए प्रस्तुत किया गया है। पुरुष की छवि ‘मोनालिसा’ के रचनाकार लियोनार्डो दा’ विंची की भी मानी जा सकती है। आकर्षण का केंद्र चित्र के साथ दिया गया वर्णन था जिसने इस आलेख के लिए प्रेरित किया। चित्र के एक पंक्ति के कैप्शन या वर्णन में इस आलेख की समूची कहानी बसी हुई है। चित्र के साथ अंग्रेज़ी में दिये गए कैप्शन मेंकहा गया है :’ This is what happens when the museum gets empty.’’
चित्र को देखते ही मैं साल 1982 के जून महीने में पहुँच गया जब लंदन में ढाई महीने गुजरने के बाद पेरिस और उसके निकट बसे ऐतिहासिक शहर ‘वर्साई’ में बिताए गए दस दिनों में न जाने कितनी बार तो ‘एफ़िल टावर’ को देखा होगा और न जाने कितनी देर तक ‘मोनालिसा’ की अद्भुत कृति को ‘लूवर म्यूज़ियम’ में निहारा होगा ! इसी के साथ 2004 में पढ़ा गया Dan Brown का प्रसिद्ध उपन्यास ‘The Da Vinci Code’ भी स्मृतियों में जीवंत हो उठा । इस पर एक चर्चित फ़िल्म भी बन चुकी है जिसमें टॉम हैंक्स ने अद्भुत अभिनय किया है।उपन्यास ‘मोनालिसा’ के रचनाकार Da Vinci और उसी म्यूजियम पर केंद्रित है जिसमें उनकी ख्यात पेंटिंग प्रदर्शित है।
पेरिस और ‘मोनालिसा’ की बात तो सिर्फ़ 42 साल पुरानी हुई। ‘मोनालिसा’ के बहाने मैं साठ साल पहले की गई मथुरा-वृंदावन-नंदगाँव-बरसाना की यात्राओं की स्मृतियों में भी टहलने लगा। बात यात्राओं की नहीं उनके बहाने कुछ अलग कहने की है !
विचार यह आया कि जिस तरह पेड़-पौधों में प्राण होने और उनके आपस में संवाद करने के आख्यान सुनने में आते हैं ,संग्रहालयों में टंगी पेंटिंग्स (जो ख्यात पेंटरों ने जीवित पात्रों को सामने बैठाकर बनाई होंगीं) वे भी सब कुछ बंद हो जाने के बाद रात के सन्नाटों में अपनी फ़्रेम्स की चौखटों से बाहर निकलकर आपस में प्रेम करती होंगी, अपने दुख-दर्द आपस में बाँटती होंगी ? ‘मोनालिसा’ दा विंची के सांसारिक जीवन का पात्र रहीं हैं। उनका असली नाम Lisa Gerardini था।
ऐसा ही संवाद विभिन्न कालखंडों में तराशी गई प्राचीन मूर्तियों और गुफाओं की चट्टानों के बीच भी होता होगा ? कहा नहीं जा सकता कि सूने जंगलों में पेड़ों के आपस में टकराने से धधकने वाली आग और उसकी लपटों के बस्तियों तक पहुँचने के पीछे क्या रहस्य छुपे हुए होंगे !
बहुत सारे लोग शायद साठ साल पहले के वृंदावन की कल्पना नहीं भी कर पाएँ ! मैं यहाँ सिर्फ़ उस ‘कुंज’ या ‘निधि वन’ की चर्चा करना चाहता हूँ जो कई छोटे-छोटे पेड़ों, लताओं से अच्छादित था।निश्चित ही आज भी वैसा ही होगा। ‘कुंज’ में भ्रमण के दौरान मुझे बताया गया था कि भगवान कृष्ण आज भी रात्रि के प्रहरों में राधारानी और गोपियों के साथ रास रचाने अवतरित होते हैं और वहाँ बने महल में विश्राम करते हैं। गाइड ने मुझे चेताया था कि रात्रि के दौरान कोई भी बाहरी व्यक्ति ‘निधि वन’ में प्रवेश नहीं कर पाता है !
सोचता हूँ कि ‘मोनालिसा’ अगर रात के सन्नाटे में पेंटिंग की चौखट से बाहर निकलकर प्रेम करती है, पेड़-पौधे आपस में बातचीत करते हैं, मूर्तियाँ और चट्टानें एक-दूसरे से संवाद करती हैं तो फिर कृष्ण भी रास रचाने अवश्य ही वृंदावन के ‘निधि वन’ में आते होंगे !
अरविंद दास
लेखक-पत्रकार
गुलजार ने एक बार कहा था कि ‘साहित्य वाले मुझे सिनेमा का आदमी समझते हैं और सिनेमा वाले साहित्य का।’ हो सकता है कि इस कथन में सच्चाई हो पर, हम जैसे साहित्य और सिनेमा प्रेमियों के लिए दोनों में कोई अंतर्विरोध नहीं है।
हाल ही में 90 साल पूरे करने वाले गुलजार 60 साल के अपने रचनात्मक जीवन में विभिन्न रूपों मसलन, कवि-लेखक, गीतकार, फिल्म निर्देशक, बच्चों के रचनाकार के रूप में अपनी सतत मौजूदगी के कारण नाम से आगे बढ़ कर एक विशेषण बन चुके हैं। गुलजार के ये ‘अपरूप रूप’ विभिन्न जबानों में छंद और अलंकार बन कर हमारे सामने आते रहे, जिनमें हम अपने जीवन का अर्थ ढूंढ़ते रहे।
जीवन भी तो एक वाक्य ही है-- कभी अधूरा तो कभी पूरा। उन्हीं के शब्दों में-‘दो नैना एक कहानी, थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी’। उनके नज्मों की खूबसूरती उनके अल्फाज में हैं। कभी हमें वे हंसाते हैं, तो कभी रुलाते हैं और कभी बस एक फरियाद बन कर हमसे गुफ्तगू करते हैं।
प्रसंगवश, यह उसी मासूम (1983) फिल्म का गाना है, जिसके किरदारों के लिए गुलजार ने ‘लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा’ अमर गीत लिखा है। उत्तर भारत के घरों में पिछले चालीस सालों में यह गीत बड़े-बूढ़ों की तरह मौजूद रहता आया है।
आजाद भारत में सामाजिक-सांस्कृतिक बदलावों के बीच गुलजार की मौजूदगी एक बुर्जुग की तरह हमारे लिए आश्विस्तिपरक है। यदि हम गुलजार के गीतों को ध्यान से सुनें तो उनमें सामाजिक-राजनीतिक बदलावों की अनुगूंज सुनाई देगी। उनकी फिल्मों आँधी, माचिस, हू तू तू आदि में यह और भी मुखर होकर सामने आया है। उनकी राजनीतिक चेतना नेहरू युग के आदर्शों से बनी है। यहाँ सांप्रदायिकता का विरोध है और सामासिकता का आग्रह।
बहरहाल, हम यहाँ उनके गीतकार रूप की ही बात करते हैं क्योंकि विभिन्न पीढ़ी के युवाओं के लिए उनके गीतों का रोमांस सबसे ज्यादा है। प्रेम उनके गीतों का स्थायी भाव है।
हम जानते हैं कि गुलजार ने ‘बंदिनी (1963)’ फिल्म में एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में ‘मोरा गोरा अंग लइ ले/मोहे शाम रंग दइ दे/छुप जाऊँगी रात ही में/ मोहे पी का संग दइ दे’ गीत रच कर अपनी सिनेमाई यात्रा शुरू की, लेकिन पिछली सदी के सत्तर-अस्सी के दशक में आरडी बर्मन के संग मिलकर उन्होंने जो रचा है वह देश-काल की सीमा के पार जा कर आज भी कानों में मिसरी घोलता रहता है और आंखों में ख्वाब के दिए जलाता रहता है।
खुसरो, गालिब और मीर की बातें करते-करते न जाने चुपके से कब वे कह देते हैं कि ‘तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं’। इस गाने में जो रोमांस है वह गुलजार आगे बयां करते हैं यह कह कर कि ‘रात को रोक लो, रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं।’ याद कीजिए कि कवि घनानंद ने कविता के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ‘लोग है लागि कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत’। बाकी लोगों के लिए कविता बनाने की चीज है, पर घनानंद की तरह ही गुलजार के लिए कविता (गीत) ही जीवन है।
इस गीतमय जीवन में बच्चों की निश्छलता है। तभी उम्र के इस पड़ाव पर भी बच्चों के लिए किताब में वे लिख सकते हैं- ‘थोड़े से तो पुराने हैं, लगते क़दीम हैं/ कहते हैं पर अण्टा गफ़़ील अच्छे हकीम हैं।’ बच्चों के लिए ही नहीं, जब वे युवाओं के लिए भी लिखते हैं तब उसी सहजता से जिसके लिए कबीर ने कहा है- ‘सहज सहज सब कोई कहै, सहज न चीन्हैं कोय।’ ‘मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है/ सावन के कुछ भीगे-भीगे दिन रखे हैं/ और मेरे इक खत में लिपटी रात पड़ी है/ वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो’, वे ही लिख सकते हैं। मनोभावों की सहज अभिव्यक्ति है यहाँ।
इस गाने को जब उन्होंने अपने मित्र आरडी बर्मन को संगीतबद्ध करने कहा तब उन्होंने झुंझला कर कहा था कि क्या वे अखबार की सुर्खियों पर अब उनको गीत कंपोज करने कहेंगे! यह असल में दो प्रगाढ़ मित्रों का आपसी नोंक-झोंक थी, जो वर्षों से चला आ रही थी। इसे आप गीत कहें, कविता या सुर्खियाँ पर इसे गाने के लिए आशा भोंसले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
गीत-संगीत और उनका परदे पर फिल्मांकन हिंदी सिनेमा को विशिष्ट बनाता है। जाहिर है गीत सिनेमा की कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं और किरदारों की पहचान बन कर आते हैं। हिंदी सिनेमा का सौभाग्य है कि उसे शैलेंद्र के बाद गुलजार जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी सर्जक ने अपने शब्दों से ‘गुलजार’ किया है। उनके लिखे गीतों का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है।
बात आजाद भारत में जवान होने वाली पीढ़ी की ही नही है, बल्कि ‘मिलेनियल’ की भी है जो कभी ‘छैंया, छैंया’ गाने पर तो कभी ‘कजरा रे कजरा रे’ गाने पर झूमती मिलती है। और हां, जब बात ‘जय हो’ की हो तो फिर ‘कहना ही क्या!’ कभी-कभी वे ‘पर्सनल से सवाल भी करती है’, लेकिन सवालों के जवाब भी हमें गुलजार ही देते हैं यह कहते हुए कि ‘पीली धूप पहन के तुम देखो बाग में मत जाना’।
गुलजार के गीत विभिन्न पीढिय़ों के बीच संवाद करती है। संवादधर्मिता गुलजार की सबसे बड़ी विशेषता है।
- स्नेहा
श्वेता को डांस करना काफी पसंद है और वो अपना छोटा-छोटा वीडियो इंस्टाग्राम पर डालती हैं। उनका कहना है कि ये एक ऐसी चीज है, जिससे उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है।
लेकिन एक दिन जब उन्होंने अपनी तस्वीर के साथ इंस्टाग्राम पर कुछ अश्लील बातें लिखी देखीं तो वो हक्की-बक्की रह गईं।
पोस्ट हटने में भी कई दिन लग गए। इस घटना ने उन्हें अंदर से हिला दिया। वो अब डिजिटल स्पेस में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं।
महिलाओं की बराबरी की राह में डिजिटल बराबरी और सुरक्षित स्पेस को अहम माना गया है लेकिन डिजिटल हिंसा ने इस राह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
26 अगस्त को वीमेन्स इक्वालिटी डे (महिला समानता दिवस) के तौर पर मनाया जाता है। अमेरिका में 26 अगस्त 1920 को संविधान में संशोधन कर महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार देने की घोषणा हुई थी।
आइए जानते हैं क्या है डिजिटल हिंसा और इसका सामना करने की स्थिति में कौन से कदम उठाने चाहिए।
डिजिटल हिंसा क्या है?
भारत में डिजिटल क्रांति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल और इंटरनेट पहुंचा। इसने लोगों को बेशक जागरूक और सशक्त किया लेकिन इस डिजिटल दुनिया में भी हिंसा का वो रूप रिस-रिसकर पहुंचा जिसका सामना वर्षों से असल दुनिया में महिलाएं कर रही थीं।
यूएन पॉपुलेशन फंड के मुताबिक़ महिलाओं और लड़कियों के मामले में ये सीधा बदनामी से जुड़ जाता है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव के साथ ही वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दुनिया में अलग-थलग पडऩे लगती हैं। इसका कार्यस्थल, स्कूल या लीडरशिप पॉजिशन पर उनकी हिस्सेदारी में असर पड़ता है।
ऑनलाइन हैरेसमेंट, हेट स्पीच, तस्वीरों से छेड़छाड़, ब्लैकमेल, ऑनलाइन स्टॉकिंग, अभद्र सामग्रियां भेजना समेत कई चीजें डिजिटल वॉयलेंस का हिस्सा हैं। एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के साथ इसके ख़तरे और भी बढ़ गए हैं।
यूएन के अनुसार, एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा की गई वैसी हिंसा जिसकी जड़ें लैंगिक असमानता और लैंगिक भेदभाव में धंसी हुई हों और जिसे अंजाम देने में या बढ़ावा देने में डिजिटल मीडिया या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो, वो इसके दायरे में हैं।
द इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट के एक सर्वे के अनुसार, दुनिया भर में 85 प्रतिशत महिलाओं ने किसी न किसी फॉर्म में ऑनलाइन हिंसा का सामना किया।
भारत में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध के मामले कोविड के बाद ज़्यादा दर्ज हुए हैं। इस अपराध में ब्लैकमेलिंग/बदनाम करना/तस्वीरों के साथ छेड़छाड़/अभद्र सामग्री भेजना/फेक प्रोफाइल जैसी चीजें शामिल हैं।
श्वेता के मामले में उनकी तस्वीरें अपलोड करनेवाले को वो नहीं जानती थीं। उन्होंने पोस्ट को रिपोर्ट किया, जिसके बाद वो हट गया। लेकिन रिमझिम के केस में ऐसा नहीं था।
रिमझिम का कहना है कि उनके साथ जो हुआ, अगर उसमें उनके परिवारवालों का साथ नहीं मिला हुआ होता तो वो ये कानूनी लड़ाई कभी लड़ ही नहीं पातीं।
उनका दावा है कि उनके एक जानने वाले ने ही उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया, जब उन्होंने आईडी रिपोर्ट की तो उसने कई आईडी बनाकर उन्हें परेशान और ब्लैकमेल करना शुरू किया।
रिमझिम कहती हैं कि एक बात गौर करने वाली थी कि अभियुक्त को इस बात का पूरा भरोसा था कि उसका कुछ नहीं होगा और इनकी (रिमझिम) की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
रिमझिम और श्वेता के मामले में एक चीज कॉमन है कि उनके दिलो-दिमाग में इसकी छाप लंबे समय तक बनी रही। उन्हें लंबा वक़्त इससे उबरने में लगा।
कानून में इसके लिए क्या हैं प्रावधान?
बीबीसी ने जब इस बारे में पेशे से वकील सोनाली कड़वासरा से बातचीत की तो उनका कहना था कि भारत में इसके लिए कानून हैं लेकिन दिक्कत मामलों का लंबा चलना है।
वो कहती हैं कि डिजिटल हिंसा से निपटने के लिए भारतीय कानून में कई प्रावधान हैं। सबसे पहले तो ये दो चीजें करनी चाहिए।
आप जिस भी सोशल मीडिया पर हों वहां संबंधित आईडी को ब्लॉक करने का ऑप्शन आपके पास होता है, आप वहां इसे रिपोर्ट भी कर सकती हैं।
ये अपराध ‘साइबर क्राइम’ के दायरे में आते हैं, आप राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन मामला दर्ज करा सकती हैं।
सोनाली कड़वासरा के अनुसार, ‘कानून में कई सारे प्रावधान हैं। ये नए नहीं हैं, पहले से हैं। आईटी एक्ट में सेक्शन 66, 67, 71 ये सभी हैं, जो आपको डिजिटल हिंसा के खिलाफ सुरक्षा देते हैं। अगर किसी ने अपने असली नाम से आईडी बनाई है, जिससे वो आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है या आपको गंदे मैसेज कर रहा है या कुछ ऐसा है जो आपको डिफेम कर रहा हो तो आईटी एक्ट के साथ आप शिकायत दर्ज करा सकती हैं।’ अनजान व्यक्ति के केस में आप उस व्यक्ति की आईडी बताकर भी शिकायत दर्ज कर सकती हैं।
सोनाली कड़वासरा कहती हैं, ‘भारत में इस मामले में प्रावधान की दिक्कत नहीं है। मेरा मानना है कि दिक्कत मामलों के निपटारे में है। इसके लिए कुछ नया लाने की जरूरत है। जैसे अभी के समय में अपनी पहचान छिपाकर एक आईडी बना लेना और उससे किसी को परेशान करना बहुत ही आसान है। बिना पहचान जाहिर किए आईडी बनाने को थोड़ा मुश्किल किया जाए। ताकि उस व्यक्ति तक जल्दी पहुंचने में आसानी हो।’
‘पुलिस को ऐसे मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेप हो या मर्डर हो तभी उनकी आंखें खुले। छोटी चिंगारी को भी उन्हें उतनी ही गंभीरता से लेने ज़रूरत है। छोटी-छोटी चीजें ही बड़े क्राइम का रूप ले लेती हैं। ’
मानसिक सेहत पर असर
रिमझिम कहती हैं, ‘मैं घंटों रोती रहती थी, हमेशा ये सोचती रहती थी कि जिसकी नजर भी उस पोस्ट पर पड़ी होगी, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। मैं सोचती थी कि क्या कोई रास्ता है कि मैं इस ब्लैकमेलिंग से बाहर निकल सकूं, मुझे बस अंधेरा ही अंधेरा दिखता था। मुझे पुलिस के पास भी जाने से डर लगता था कि कंप्लेन की बात एक दिन की तो है नहीं। मैं पढ़ाई करूं, नौकरी के बारे में सोचूं, मेरी शादी फिक्स हो रही थी, उस पर ध्यान दूं।’
रिमझिम ने एक दिन साहस कर जब परिवारवालों को बताया और उनके कहने पर वो पुलिस के पास गईं। (बाकी पेज 8 पर)
लेकिन इन सब के बीच वो मानसिक तनाव में डूबती गईं। वो कहती हैं, ‘पहले मुझे लगता था कि ये मामला ज़्यादा से ज़्यादा साल भर लंबा चलेगा लेकिन साल दर साल ये लंबा खिंचता गया और मैं मानसिक तौर पर परेशान होती गई।’
क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजाशिवम जेटली कहती हैं कि पितृसत्तात्मक समाज में जिस तरीके का पावर बाहरी दुनिया में दिखता है, वही ऑनलाइन स्पेस में भी मिलता है। ऑनलाइन स्पेस में लोग ये भी महसूस करते हैं कि वो कुछ भी बोल और किसी को कुछ भी कह सकते हैं।
‘अगर कोई महिला अपने काम के बारे में भी वहां बता रही हो तो आप देखोगे कि उस पर सेक्सुअल कमेंट्स, बॉडी शेमिंग की जाती है। खासतौर पर टीएनजर्स (किशोरी) लड़कियां इसका ज्यादा शिकार हो रही हैं।’
पूजाशिवम जेटली कहती हैं, ‘मेरे पास इस तरह के मामलों में मदद के लिए ज़्यादातर किशोरी लड़कियां आती हैं। उनके लिए डिजिटल दुनिया एक ऐसी दुनिया होती है, जहां वो अपना काफी समय बिताती हैं, अगर वो वहां हैरेसमेंट, बुलिंग की समस्या का सामना करती हैं तो वो काफी उहापोह की स्थिति में आ जाती हैं कि हेल्प किससे मांगें, क्या करें और उन्हें लगता है कि अगर यहां से हटे तो एक तरह से अपने दोस्तों और अपने ग्रुप से कट आउट हो जाएंगे।’
इससे कैसे निपटें, वो बताती हैं-
ब्लॉक करना, इग्नोर करना-अच्छा उपाय है
एक उपाय ये भी है कि उस कमेंट्स को आप शेयर करें, इससे आपको अपने सपोर्ट ग्रुप का समर्थन मिलता है।
कभी-कभी कुछ लोगों को डिजिटल स्पेस में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऐसे में वहां से कुछ समय के लिए स्विच ऑफ़ होना भी एक उपाय है ताकि मानसिक शांति रह सके।
वही चीजें शेयर करें, जिसमें आप कंफर्टेबल हों।
अकाउंट को प्राइवेट रखना भी एक बेहतर विकल्प है
सीमित इस्तेमाल
कोई चीज जो हमें लगातार परेशान कर रही है तो उस स्थिति में वहां से बाहर निकल जाना चाहिए, जब हम किसी चीज को बार-बार देखते हैं तो उसका और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
जहां जरूरत लगे प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए।(bbc.com/hindi)
-भाग्यश्री राउत
हाल के वक्त में कोलकाता में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया।
ये मामला थमा ही नहीं था कि महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में दो नाबालिग़ों के साथ यौन शोषण और अकोला में स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की ख़बर आई।
आम जनता ने सडक़ों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने दोषियों के ख़िलाफ़ सख़्त रुख़ अपनाया और उनके लिए फांसी की मांग की।
इसी माहौल के बीच बुधवार को एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अनुसार 151 मौजूदा विधायकों और सांसदों के ख़िलाफ़ महिला उत्पीडऩ के मामले दर्ज हैं।
300 पन्नों की इस रिपोर्ट में कितने सांसदों, विधायकों पर महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध, बलात्कार के आरोप लगे हैं इसकी जानकारी है। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि कितने विधायक और सांसद किस पार्टी से हैं।
इस रिपोर्ट के लिए एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने संयुक्त रूप से देश के कुल 4,809 मौजूदा सांसदों और विधायकों में से 4,693 के चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफऩामों का अध्ययन किया है।
इन हलफऩामों से विधायकों और सांसदों ने अपने ख़िलाफ़ दर्ज किए गए अपराधों की जानकारी दी है। इसमें 776 मौजूदा सांसदों में से 755 और 4,033 विधायकों में से 3,938 के हलफऩामे शामिल हैं।
एडीआर और इलेक्शन वॉच ने ये जानकारी 2019 से 2024 के बीच हुए उप-चुनावों समेत सभी चुनावों के दौरान दर्ज किए गए हलफऩामों से जुटाई है।
कौन से अपराध शामिल हैं?
इस रिपोर्ट में विस्तार से जानकारी दी गई है कि किन सांसदों और विधायकों पर महिला उत्पीडऩ के अपराध दर्ज किए गए हैं।
इनमें महिला पर एसिड अटैक, बलात्कार, यौन उत्पीडऩ, छेड़छाड़, किसी महिला को निर्वस्त्र करने के उद्देश्य से उस पर हमला करना, किसी महिला का पीछा करना, वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग़ लड़कियों को खरीदना और बेचना, पति या ससुराल के रिश्तेदारों के हाथों महिला का उत्पीडऩ, इरादतन किसी शादीशुदा महिला को जबरन रोकना या अगवा करना, महिला की सहमति के बिना जबरन उसके साथ रहना, पहली पत्नी के रहते अन्य महिला से शादी करना और दहेज हत्या शामिल है।
कितने विधायकों, सांसदों पर महिला उत्पीडऩ के मामले दर्ज हैं?
755 सांसदों और 3,938 विधायकों में से 151 विधायकों और सांसदों ने अपने हलफऩामे में महिला उत्पीडऩ से जुड़े दर्ज अपराधों की जानकारी दी है।
इसमें 16 मौजूदा सांसद और 135 मौजूदा विधायक शामिल हैं।
हलफऩामे में जिन अपराधों की बात की गई है उनमें बलात्कार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, छेड़छाड़, वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग़ लड़कियों की खरीद-फरोख्त, घरेलू हिंसा जैसे अपराध शामिल हैं।
किस पार्टी के कितने जनप्रतिनिधियों पर हैं मुक़दमे?
कुल 151 जन प्रतिनिधि जिनपर महिला हिंसा से जुड़े अपराध के मामले चल हैं उनमें से किस पार्टी के कितने प्रतिनिधि हैं इसकी भी जानकारी एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट में दी गई है।
इसमें 135 विधायक हैं जबकि 16 सांसद हैं जिनके ख़िलाफ महिला अपराध के मामले चल रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा 54 बीजेपी के जन प्रतिनिधि हैं। वहीं कांग्रेस के 23, तेलुगु देशम पार्टी के 17, आम आदमी पार्टी के 13, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के 10, पांच राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी के ज़्यादातर जन प्रतिनिधियों पर (44 विधायक और 10 सांसद) महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के आरोप लगे हैं।
लेकिन, इस वक्त देश में बीजेपी विधायकों-सांसदों की संख्या अधिक है। इसलिए बीजेपी नेताओं को लगता है कि इस वजह से ये संख्या ज़्यादा हो सकती है।
बीजेपी विधायक देवयानी फरांदे ने बीबीसी से कहा, ‘कई बार राजनीतिक द्वेष के कारण नेता के ख़िलाफ़ अपराध दर्ज कराए जाते हैं। लेकिन महिला उत्पीडऩ की घटना बेहद अफ़सोसजनक है। महिलाओं पर अत्याचार का का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।’
वो कहती हैं कि ‘महिला उत्पीडऩ को लेकर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं के नामांकन के समय उनके व्यक्तित्व की जांच की जानी चाहिए जिसके बाद ही उम्मीदवारी की अनुमति दी जानी चाहिए।’
किस राज्य में सबसे अधिक सांसदों पर महिला अपराध के आरोप
एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने अपनी रिपोर्ट में विधायकों और सांसदों की संख्या राज्यवार जानकारी दी है। इसके अनुसार पश्चिम बंगाल और उसके बाद आंध्र प्रदेश में ऐसे जन प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक जिन पर महिलाओं के साथ अपराध के आरोप लगे हैं।
पश्चिम बंगाल में यह संख्या 25 (21 विधायक, 4 सांसद), आंध्र प्रदेश में 21 (21 विधायक), ओडिशा में 17 (16 विधायक, सांसद 1), दिल्ली और महाराष्ट्र में 13 (दिल्ली में 13 विधायक, महाराष्ट्र में 12 विधायक और 1 सांसद) शामिल हैं।
इसके अलावा बिहार में 9, कर्नाटक में 7, राजस्थान में 6, मध्य प्रदेश, केरल और तेलंगाना में 5-5, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 4-4, झारखंड और पंजाब में 3-2, असम और गोवा में 2-2 और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, दादरा नगर हवेली और दमन दीव में एक-एक जन प्रतिनिधि पर महिला उत्पीडऩ के मामले हैं।
कितने जन प्रतिनिधियों पर बलात्कार के मामले दर्ज हैं?
एडीआर और इलेक्शन वॉच ने चुनाव आयोग को दिए गए उम्मीदवारों के हलफऩामों के विश्लेषण से पाया कि जिन 151 जन प्रतिनिधियों के ख़िलाफ महिला उत्पीडऩ के आरोप हैं, उनमें से 16 के ख़िलाफ बलात्कार के मामले हैं। इनमें 2 सांसद और 14 विधायक हैं।
राज्यवार देखा जाए तो इसमें मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। प्रदेश के दो जनप्रतिनिधियों पर बलात्कार के अपराध दर्ज हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के एक सांसद पर इस तरह का आरोप दर्ज है।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु के एक-एक जनप्रतिनिधि पर बलात्कार का आरोप लगा है। वहीं तेलंगाना के एक सांसद पर बलात्कार पर अपराध दर्ज है।
पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो जिन जनप्रतिनिधियों पर बलात्कार के मामले दर्ज हैं उनमें सबसे अधिक बीजेपी के 5 (3 विधायक, 2 सांसद) और कांग्रेस के 5 विधायक शामिल हैं।
इसके अलावा आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ़), भारत आदिवासी पार्टी और बीजू जनता दल (बीजेडी) के एक-एक विधायक के ख़िलाफ़ बलात्कार का मामला है।
रिपोर्ट में उन नेताओं के नाम भी दिए गए हैं जिनके खिलाफ यौन हिंसा के मामले दर्ज है। इनमें से कई नेताओं पर आरोप लगने के बाद मामला दर्ज किया गया, लेकिन रिपोर्ट बनाए जाने तक आरोप तय नहीं हुए। कुछ मामलों की सुनवाई अभी भी जारी है।
इनमें से हर नेता ने उस समय अपने ख़िलाफ़ लगे आरोपों से इनकार किया है। हालांकि नेताओं ने चुनाव आयोग को दिए हलफऩामे में अपराधों की जानकारी दी है।
‘जब क़ानून बनाने वाले ही अपराधी, तो न्याय की उम्मीद किससे करें?’
एक तरफ जब देश में महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा की घटनाएं रुक नहीं रहीं और महिला सुरक्षा को लेकर बहस चल रही है, ऐसे में देश के चुने हुए नेताओं के बारे में इस तरह की रिपोर्ट के बारे में महिला राजनीतिक विश्लेषक क्या सोचती हैं?
वरिष्ठ पत्रकार प्रतिमा जोशी ने बीबीसी से कहा, ‘ऐसा नहीं है कि ऐसे जन प्रतिनिधि हाल ही में राजनीति में आए हैं। ये धीरे-धीरे बढ़ता गया है। हम सत्ता में रहते हुए आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों से न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं।’
वो कहती हैं, ‘बिलकिस बानो के मामले में अभियुक्तों को समयसीमा ख़त्म होने से पहले आज़ाद कर दिया गया। यह बेशर्मी की पराकाष्ठा है। ऐसा लगता है कि शासक वर्ग ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति वालों को पनाह दे रहा है।’
‘आम महिलाएं किससे न्याय की उम्मीद करें? इस प्रवृत्ति ने राजनीति से महिलाओं की संख्या कम कर दी है।’ वहीं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी का मानना है कि ऐसे नेताओं को टिकट देना सभी राजनीतिक दलों का पाखंड है।
उन्होंने बीबीसी से कहा, ‘जिन विधायकों और सांसदों के ख़िलाफ़ महिला उत्पीडऩ अपराध हैं उनकी संख्या काफी बड़ी है। राजनीतिक दल पार्टी के बड़े नेताओं को चुनाव के लिए टिकट देते हैं। हालांकि, उनके ख़िलाफ़ जो अपराध दर्ज होते हैं उन्हें नजऱअंदाज कर दिया जाता है।’
‘ये चिंता का विषय है कि महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध दर्ज होने पर भी चुनाव लडऩे के लिए टिकट देना कितना उचित है?’
नीरजा कहती हैं ‘एक तरफ राजनीतिक दल खुद न्याय की बात करते हैं, हकों के लिए आवाज़ उठाते हैं और दूसरी तरफ आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को मैदान में उतारते हैं। यह सभी राजनीतिक दलों का पाखंड है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि 2024 के भारत में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं।’
विदेशों में नौकरी की तलाश करने वाले नेपाली पारंपरिक रूप से एशिया के नजदीकी देशों के साथ-साथ कतर या दुबई जैसे अरब देशों में जाते रहे हैं. यह रुझान बदलता हुआ दिख रहा है. अब यूरोप उनका पसंदीदा ठिकाना बनता जा रहा है.
 डॉयचे वैले पर स्वेच्छा राउत का लिखा-
डॉयचे वैले पर स्वेच्छा राउत का लिखा-
दक्षिण एशिया के नेपाल के पंचथर जिले के नरेंद्र भट्टाराई 2007 में बेहतर अवसर की तलाश में कतर चले गए थे। इससे पहले वह अपने देश में एक लेखक, कवि और महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता के तौर पर आजीविका चला रहे थे। भट्टाराई ने कतर जाने की योजना सावधानी से बनाई। उन्होंने एक एजेंट को काफी पैसे दिए, ताकि उन्हें ज्यादा वेतन वाली ड्राइवर की नौकरी मिल सके।
हालांकि, वहां पहुंचने पर उन्हें निर्माण कार्य में श्रमिक के तौर पर काम करने को मजबूर किया गया। विदेश जाने से पहले उन्हें हर महीने 900 कतरी रियाल, यानी करीब 247 डॉलर मिलने की गारंटी दी गई थी, लेकिन सिर्फ 600 रियाल ही मिले। भट्टाराई ने डीडब्ल्यू को बताया, मैंने अपने परिवार को बेहतर जीवन देने का सपना देखा था, लेकिन मैं शोषण का शिकार हो गया।
भट्टाराई को अपना कर्ज चुकाने के लिए कतर में कई सालों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इसके बाद वह फिर से नेपाल लौट आए। कविता और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में काम करना शुरू किया और पैसे कमाने का उनका संघर्ष जारी रहा।
भारत के लोगों का नया ठिकाना बन रहा है पुर्तगाल
2019 में वह एक फिल्म स्क्रीनिंग के लिए पुर्तगाल की यात्रा कर रहे थे। इस दौरान उन्हें पता चला कि वह वहां रहने के लिए आवेदन कर सकते हैं और यूरोपीय संघ के देश में कानूनी रूप से काम कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। भट्टाराई ने डीडब्ल्यू से कहा, यूरोप में लंबे समय तक रहने का मतलब है कि मेरे और मेरे परिवार का भविष्य बेहतर हो सकता है।
पुर्तगाल ने बाहरी लोगों के लिए अपना दरवाजा खोला
भट्टाराई उन सैकड़ों नेपालियों में से एक थे, जिन्हें 2019 में पुर्तगाल में काम मिला। नेपाल सरकार के आधिकारिक डेटा से पता चलता है कि 2018 में केवल 25 लोगों को पुर्तगाली वर्क परमिट मिला था, लेकिन अगले वर्ष यह संख्या बढक़र 461 हो गई।
यूरोपीय अध्ययन 'रीथिंकिंग अप्रोच टू लेबर माइग्रेशन - फुल केस स्टडी पुर्तगाल' के अनुसार, पुर्तगाल को कम कौशल वाले कामगारों की जरूरत थी और वह उन्हें 'विशेष रूप से कृषि और पर्यटन' क्षेत्र में नौकरी करने की अनुमति दे रहा था। 2019 से 2024 के बीच, कई यूरोपीय देशों ने बताया कि उनके यहां नेपाली कामगारों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। रोमानिया में नेपाली कामगारों की संख्या सबसे ज्यादा 640 फीसदी बढ़ी।
यूरोप क्यों हो रहा ज्यादा लोकप्रिय
कुवैत जैसे देशों में भी इस अवधि में नेपाली कामगारों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल के कामगारों के प्रवासन का ढर्रा बदल रहा है। एशिया और फारस की खाड़ी के आसपास के पारंपरिक ठिकानों को छोडक़र कई कामगार पोलैंड, रोमानिया, पुर्तगाल, माल्टा, हंगरी, क्रोएशिया और अन्य यूरोपीय देश जा रहे हैं।
कुशल कामगारों के लिए जर्मनी आना हुआ और आसान
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यहां उन्हें कमाई के बेहतर अवसर मिल रहे हैं और आसानी से नौकरियां भी मिल रही हैं। समाजशास्त्री टीकाराम गौतम ने डीडब्ल्यू को बताया, हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक ढांचे ने भविष्य के लिए बचत करने की हमारी मानसिकता को बढ़ावा दिया है। वैश्वीकरण की वजह से कामगारों को कई तरह के विकल्प मिल रहे हैं। इसलिए वे ऐसे देश में जाना चाहते हैं, जहां अधिक कमाई कर सकें। हालांकि, सामाजिक प्रतिष्ठा और साथियों का दबाव भी एक बड़ी वजह है।
पुर्तगाल के ओदेमिरा नाम की जगह पर सडक़ किनारे एक बेंच पर बैठे कुछ एशियाई प्रवासी। यह इलाका खेती का एक अहम केंद्र है। बसंत का मौसम आते-आते भारत और नेपाल से हजारों की संख्या में कामगार यहां कृषि क्षेत्र में काम करने आते हैं। पुर्तगाल के ओदेमिरा नाम की जगह पर सडक़ किनारे एक बेंच पर बैठे कुछ एशियाई प्रवासी। यह इलाका खेती का एक अहम केंद्र है। बसंत का मौसम आते-आते भारत और नेपाल से हजारों की संख्या में कामगार यहां कृषि क्षेत्र में काम करने आते हैं।
नेपाल में जन्मे दीपक गौतम पिछले एक दशक से दुबई में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम कर रहे हैं। वह इतना कमा लेते हैं कि अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा घर भेज पाते हैं। हालांकि, उनका कहना है कि यूरोप में काम न करने के कारण उन्हें नीची नजरों से देखा जाता है। यानी, समाज में उन्हें ज्यादा प्रतिष्ठा नहीं मिलती है।
उन्होंने बताया, नेपाली समाज में यूरोप में काम करना प्रतिष्ठित माना जाता है, जबकि खाड़ी में काम करने वाले हम लोगों को असफल माना जाता है। नेपाली समाज यह मानता है कि यूरोप में काम करने के हालात बेहतर हैं, वहां ज्यादा वेतन मिलता है और काम के ज्यादा अवसर उपलब्ध हैं। दीपक कहते हैं कि उन्होंने पोलैंड के वर्किंग वीजा के लिए आवेदन करने की कोशिश की, लेकिन दो बार उन्हें अस्वीकार कर दिया गया।
नेपाल क्यों छोड़ रहे हैं युवा कामगार
अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) के मुताबिक, नेपाल की जीडीपी में 26।6 फीसदी योगदान उन पैसों का है जो विदेशों में काम करने वाले कामगार अपने घर भेजते हैं। 2023 में इसका अनुमानित मूल्य 11 अरब डॉलर था।
दरअसल, हिमालय की गोद में बसे इस देश में राजनीतिक उथल-पुथल, कमजोर अर्थव्यवस्था, बड़े पैमाने पर रोजगार से जुड़ी योजनाओं की कमी, और मानव संसाधन का सही तरीके से प्रबंधन न हो पाने की वजह से यहां के लोग रोजी-रोटी के लिए दूसरे देशों का रूख करते हैं।
राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा और तकनीक तक पहुंच के मामले में यह देश अपेक्षाकृत खुला और उदार है। श्रम विशेषज्ञ मीना पौडेल के मुताबिक, इन वजहों से नेपाल के लोग जागरूक वैश्विक नागरिक बन गए हैं और सरकार से उनकी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। वह आगे बताती हैं, वे लोग वैश्विक स्तर पर हो रहे विकास के बारे में जानते हैं, लेकिन वे इन सुविधाओं की तुलना नेपाल में मिलने वाली सुविधाओं से नहीं कर सकते।
अकुशल कामगारों के लिए आसपास कम नौकरियां
हाल के वर्षों में मलेशिया या खाड़ी देशों जैसे देशों ने प्रवासी मजदूरों के लिए मानदंड बढ़ा दिए हैं। पौडेल ने बताया, नौकरी देने वाले लोग या कंपनियां भी कुशल व्यक्ति की तलाश करने लगी हैं। इससे कम कुशल या अकुशल लोग अन्य विकल्प तलाशने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
विदेशी कामगारों को आकर्षित करने के लिए टैक्स में छूट दे रहे ईयू के देश
वहीं, यूरोप के कई देशों ने अपने इमिग्रेशन कानूनों में ढील दी है। इससे विदेशी कामगारों के लिए वीजा हासिल करना आसान हो गया है, खासकर कृषि, हाउसकीपिंग, हॉस्पिटैलिटी और निर्माण कार्य जैसे क्षेत्रों में। साथ ही, यह भी माना जाता है कि यूरोप के देशों में कामगारों का शोषण कम होता है और उन्हें वहां ज्यादा आजादी भी मिलती है।
यूरोप में बेहतर जीवन के सपने को साकार करना
पिछले साल से जर्मनी अपने कुशल आप्रवासन कानून में बदलाव कर रहा है। इसके तहत, रोजगार की तलाश कर रहे तीसरे देश के नागरिकों के लिए 'अपॉरच्यूनिटी कार्ड' की योजना पेश की गई है।
जर्मनी में नौकरी पाने के सपने के साथ बिजय लिम्बू छह महीने पहले माल्टा पहुंचे थे। इससे पहले वह कतर में काम कर चुके हैं। उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, मैं अपने कौशल को बेहतर बना रहा हूं और भाषा सीख रहा हूं, ताकि रेजिडेंस परमिट से जुड़ी शर्तें पूरी कर सकूं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि प्रवासियों का काम हमेशा अनिश्चित होता है।
नेपाली लेखक नरेंद्र भट्टाराई का नया घर पुर्तगाल इसका एक अच्छा उदाहरण है। हाल ही में हुए कानूनी बदलावों ने उन अप्रवासियों के लिए और भी बाधाएं खड़ी कर दी हैं जो इस देश में काम करना और बसना चाहते हैं। भट्टाराई कहते हैं कि वह पुर्तगाल में मानसिक और आर्थिक रूप से संतुष्ट हैं। इससे उन्हें एक बार फिर से लेखन के प्रति अपने जुनून को जगाने का मौका मिल रहा है। वह कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं सही समय पर यूरोप आया हूं। (dw.com/hi)




.jpg)