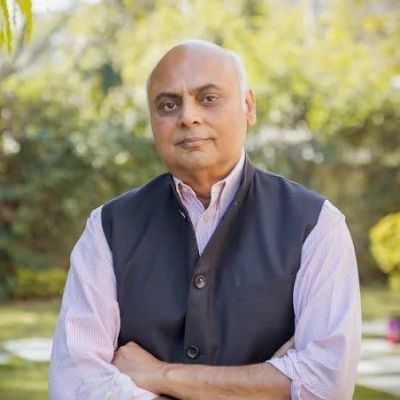विचार / लेख
-रेहान फजल
भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहाँगीर भाभा और नेहरू की पहली मुलाकात कब हुई, इसका पक्का विवरण कहीं नहीं मिलता लेकिन इंदिरा गाँधी ने बंबई में होमी भाभा ऑडिटोरियम के उद्घाटन के समय दिए भाषण में याद किया था कि उनकी भाभा से पहली मुलाकात साल 1938 में हुई थी जब वो अपने पिता के साथ पानी के जहाज़ से फ्ऱांस के शहर मारसे जा रही थीं।
नेहरू दुनिया के उन नेताओं में से एक थे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिमायती थे, इसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि भारत के आज़ाद होने के एक पखवाड़े के अंदर ही नेहरू ने भाभा के नेतृत्व में बोर्ड ऑफ़ रिसर्च ऑन एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की थी।
नेहरू और भाभा दोनों ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एमआर श्रीनिवासन ने लिखा था, ‘उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। मेरा मानना है कि महात्मा गाँधी, इंदिरा गाँधी, उनके परिवार के अन्य सदस्यों और कृष्ण मेनन को छोडक़र, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नेहरू के उतने करीब था, जितने भाभा थे।’
श्रीनिवास लिखते हैं, ‘भाभा नेहरू को हमेशा ‘भाई’ कहकर पुकारते थे। इंदिरा गाँधी का भी मानना था कि उनके पिता के पास भाभा के लिए हमेशा समय होता था, केवल इसलिए नहीं कि भाभा अहम मुद्दों पर बातें करते थे, बल्कि इसलिए कि भाभा से बातचीत कर नेहरू अच्छा महसूस करते थे। भाभा नेहरू की बौद्धिक भूख को पूरा करते थे जो राजनीति में रहने के कारण कभी पूरी नहीं हो पाती थी।’
इसका दूसरा कारण ये भी था कि दोनों की शख्सियतों में पूर्व और पश्चिम का अद्भुत समन्वय था।
साल 1954 आते-आते परमाणु ऊर्जा आयोग सरकार का एक अलग विभाग बन गया था और होमी भाभा को इसका पहला सचिव बनाया गया था, इससे पहले तक उसकी भूमिका सलाह देने तक की थी।
इसके साथ-साथ भाभा परमाणु ऊर्जा आयोग और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ फंडामेंटल रिसर्च के प्रमुख की भूमिका भी निभा रहे थे।
नेहरू और भाभा के नेतृत्व में साल 1955 में अलवाए में थोरियम प्लांट और फिर ट्रॉम्बे में पहले परमाणु रिएक्टर ने काम करना शुरू कर दिया था।
बड़ी परियोजनाओं को बताया ‘नए भारत का मंदिर’
देश के आज़ाद होते ही नेहरू ने विज्ञान से जुड़े संस्थानों की नींव डालनी शुरू कर दी थी। आज जो आईआईटी, आईआईएम, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइज़ेशन और एम्स जैसे संस्थान दिखाई देते हैं नेहरू ने इनकी शुरुआत तब की थी जब भारत के आर्थिक संसाधन बहुत सीमित थे। पहली आईआईटी साल 1952 में पश्चिम बंगाल में खडग़पुर मे बनाई गई थी। भाखड़ा में सतलज नदी पर बनाए जाने वाले बाँध को उन्होंने ‘आधुनिक भारत के नए मंदिर’ की संज्ञा दी थी। वो हर वर्ष इंडियन साइंस कांग्रेस में भाग लेते थे।
पीयूष बबेले अपनी किताब ‘नेहरू मिथक और सत्य में लिखते हैं, ‘नेहरू को देश के खेतों तक पानी पहुंचाना था, करोड़ों लोगों को रोजग़ार देना था, बच्चों को तालीम देनी थी, विज्ञान की नई से नई बात से देश को परिचित कराना था, देश की हिफाजत के लिए फौजी इंतजाम करने थे, कला -संस्कृति को बुलंदियों पर ले जाना था, विदेशी मेहमानों के लिए होटल बनाने थे, चंडीगढ़ जैसे शहर बसाने थे। कौन-सा काम था, जो उन्हें नहीं करना था? सुबह पाँच बजे से रात एक बजे तक काम करने वाले नेहरू के इरादों का क्षितिज व्यापक था। वो दूर तक देखते थे।’
राजेंद्र प्रसाद ने दिया भारत रत्न
आज़ाद भारत के पहले मंत्रिमंडल में नेहरू ने अपने कटु आलोचकों डॉक्टर भीमराव आंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जगह दी थी। ये एक अद्भुत प्रयोग था जिसे बाद का कोई प्रधानमंत्री दोहराने की हिम्मत नहीं कर सका। नेहरू मंत्रिमंडल के सदस्य रहे भीमराव आंबेडकर ने उनकी ये कहकर आलोचना की थी कि 'उन्होंने कांग्रेस को एक तरह की धर्मशाला बना दिया है जिसमें सिद्धांतों और नीतियों का कोई महत्व नहीं है। उसमें मूर्खों के लिए भी जगह है और धूर्तों के लिए भी। उसमें दुश्मन भी आ सकते हैं और दोस्त भी। कम्युनिस्टों के लिए उसके दरवाज़े खुले हैं और धर्मनिरपेक्ष लोगों के लिए भी। कांग्रेस में पूंजीवादियों के लिए भी जगह है और उसके विरोधियों के लिए भी।’
साल 1955 में जवाहरलाल नेहरू को उस समय भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी जब वो यूरोप की यात्रा पर थे। बहुत से लोगों को ये ग़लतफ़हमी है कि ये सम्मान उन्हीं की सरकार ने उन्हें दिया था।
राशिद किदवई अपनी किताब ‘भारत के प्रधानमंत्री, देश दशा दिशा’ में लिखते हैं, ‘तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के प्रधानमंत्री नेहरू के साथ कई मुद्दों पर मतभेद थे। इसके बावजूद प्रसाद ने नेहरू को भारत रत्न देने की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की थी । उन्होंने कहा, ‘चूँकि ये कदम मैंने अपने विवेक से, अपने प्रधानमंत्री की अनुशंसा के बग़ैर और उनसे किसी सलाह के बग़ैर उठाया है, इसलिए इसकी ये कहकर आलोचना की जा सकती है कि फ़ैसला असंवैधानिक है लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे इस फ़ैसले का पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया जाएगा।’
‘दिन में 17 घंटे काम करते थे नेहरू’
नेहरू बहुत मेहनती शख्स थे। वो भोर होने के तुरंत बाद उठ जाते थे और दिन में 16-17 घंटे काम करते थे। इस दौरान वो इंटरव्यू देने, बैठकों में भाग लेने, नौकरशाहों और विदेशी राजनयिकों से मिलने और संसद अगर सत्र में है तो उसकी कार्रवाई में भाग लेने का समय निकाल लेते थे। रोज़ सुबह योग करना और पाँच से दस मिनट तक शीर्षासन करना उनकी दिनचर्या में शामिल था। तैरना और घुड़सवारी करना भी उन्हें बहुत पसंद था।
उनके पहले प्रधान निजी सचिव एचवीआर आयंगर ने लिखा था, ‘अगस्त, 1947 में पंजाब के दंगाग्रस्त इलाकों के थका देने वाले दौरे के बाद हम सब करीब आधी रात को वापस दिल्ली लौटे। हमारा अगला कार्यक्रम अगले दिन सुबह 6 बजे का था। शारीरिक रूप से थका होने के कारण मैं तुरंत सोने चला गया। जब मैं सुबह हवाई-अड्डे जाने के लिए प्रधानमंत्री निवास पहुंचा तो उनके पीए ने मुझे वो पत्र, टेलीग्राम और बयान दिखाए जो नेहरू ने उस समय लिखवाए थे जब हर कोई सोने चला गया था। प्रधानमंत्री उस रात दो बजे सोने गए थे लेकिन साढ़े पाँच बजे अगला दिन शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे।’
नेहरू के करीबी दोस्त सैयद महमूद जब उनसे पहली बार मिले तो उनके ‘उच्चवर्गीय अंग्रेज़’ जैसे व्यवहार ने उन्हें बहुत प्रभावित किया लेकिन उनकी गर्मजोशी और मेहमाननवाज़ी उन्हें पूरी तरह से भारतीय बनाती थी।
सैयद महमूद ने लिखा, ‘जब भी मैं ट्रेन से सफऱ करता था अपने साथ एक नौकर को ज़रूर लेकर जाता था क्योंकि मुझे ट्रेन के बंक पर अपना बिस्तरबंद खोलना और बंद करना नहीं आता था लेकिन जब-जब मैंने जवाहरलाल के साथ ट्रेन का सफऱ किया उन्होंने मेरा होल्डाल खोलने और बंद करने की जि़म्मेदारी अपने ऊपर ले ली।’
अफसरों का काम भी ख़ुद करते थे नेहरू
मशहूर पत्रकार फ्रैंक मोरेस नेहरू की जीवनी में लिखते हैं, ‘सोने से पहले 15-20 मिनट का समय वो किताबें पढऩे में बिताते थे। उनकी पसंदीदा किताबें राजनीति, कविता, दर्शन और आधुनिक विज्ञान पर होती थीं। प्रधानमंत्री के तौर पर फ़ाइलों पर उनकी नोटिंग संक्षिप्त और स्पष्ट होती थीं। उनको जल्द-से-जल्द फाइलें निपटाने की आदत थी। उनकी मेज पर फाइलें बहुत दिनों तक नहीं रहती थीं। नेहरू बहुत ही व्यवस्थित और सफ़ाई-पसंद व्यक्ति थे। तिरछी लगी तस्वीर को सीधा करना, दोस्त के घर में मेज़ पर जमी धूल को अपने हाथों से साफ़ करना और कागज़ों और किताबों को करीने से रखना उनकी आदत में शुमार था।’
नेहरू की शख्सियत का नकारात्मक पक्ष शायद ये था कि वे देश के प्रशासन को माइक्रो-मैनेज करने की कोशिश करते थे। वो अपना बहुत अधिक समय ऐसे कामों में लगाते थे जो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए गैर-जरूरी थे।
शशि थरूर नेहरू की जीवनी ‘नेहरू, द इनवेन्शन ऑफ़ इंडिया’ में लिखते हैं, ‘नेहरू अपने सिविल सर्वेंट्स का काम खुद करना पसंद करते थे। प्रधानमंत्री के लिए ये ज़रूरी नहीं था कि वो हर पत्र का जवाब खुद लिखे लेकिन नेहरू को ऐसा करने से संतोष मिलता था। उनको अपने अफसरों से दुनिया के हर विषय पर बात करना अच्छा लगता था। रक्षा मंत्रालय में काम कर रहे एक अंग्रेज़ अधिकारी का कहना था कि जब भी मैं नेहरू के सामने जाता था वो मुझसे दुनिया के मुद्दों पर जरूर बात करते थे। मुझे ये देखकर बहुत ताज्जुब होता था कि उनके पास इन बातों के लिए समय होता था।’
नेहरू की दरियादिली और शिष्टाचार
एक बार जब घाना के नेता क्वामे इनक्रूमा जाड़े में भारत की यात्रा पर आए तो उन्होंने तय किया कि वो उत्तर भारत की यात्रा ट्रेन से करेंगे। जब इनक्रूमा की ट्रेन चलने वाली थी अचानक एक ढीला-ढाला ओवरकोट पहने नेहरू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए।
नेहरू ने इनक्रूमा से कहा, ये कोट मेरे लिए बड़ा है लेकिन ये आपको बिल्कुल फिट आएगा। आप इसको पहन लीजिए। ये आपको सर्दी से बचाएगा। जैसे ही इनक्रूमा ने कोट पहना ट्रेन चल पड़ी।
बाद में इनक्रूमा ने लिखा, ‘जैसे ही मैंने ओवरकोट की जेबों में हाथ डाला मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, कोट की एक जेब में ऊनी मफलर और दूसरे में गर्म दस्ताने रखे हुए थे।’
नेहरू का इस तरह का शिष्टाचार सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं था। शशि थरूर लिखते हैं, ‘एक बार कश्मीर की यात्रा पर उनके स्टेनोग्राफर का सूटकेस जहाज के साथ श्रीनगर नहीं पहुंचा। वो शख्स सिफऱ् सूती कमीज पहने हुए था और जाड़े में बुरी तरह से काँप रहा था। नेहरू ने सुनिश्चित किया कि उनके स्टेनो को तुरंत एक स्वेटर और जैकेट उपलब्ध कराई जाए। जेल में रहते हुए भी वो अपने साथियों का जन्मदिन नहीं भूलते थे और वहीं से उन्हें बधाई का पत्र भेजते थे।’
लोगों को पहचानने में गलती
नेहरू के बारे में उनके आलोचक कहते थे कि उन्हें लोगों की सही पहचान नहीं थी। आलोचक ही नहीं, उनकी एक दोस्त राजकुमारी अमृत कौर ने लिखा था, ‘लोगों का चरित्र पहचानने की उनकी क्षमता सटीक नहीं है। वो चापलूसी को भी प्रश्रय देते हैं जिसकी वजह से कड़ी आलोचना को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और इसकी वजह से लोगों को पहचानने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है। दोस्तों के साथ अपनी निष्ठा के कारण वो उनके दोषों की अनदेखी कर देते हैं। शायद यही वजह है कि एक नेता के तौर पर वो निर्मम नही हो पाते जिससे उनका नेतृत्व कमज़ोर होता है।’
नेहरू उन लोगों को पसंद करते थे जिनमें शारीरिक पीड़ा और तकलीफ सहन करने का साहस और सामर्थ्य हो। 12 सितंबर, 1855 को खजुराहो में जब वो कार से उतर रहे थे तो उनकी दो उंगलियाँ कार के दरवाजे में आ गई थीं। उन्होंने चोटग्रस्त उंगलियों पर पट्टियाँ बँधवा लीं और अपना दौरा पूरा करके इलाहाबाद वापस लौट गए।
पीडी टंडन अपनी किताब ‘अविस्मरणीय नेहरू’ में लिखते हैं, ‘उस दिन नेहरू ने सबसे हाथ मिलाने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। उनकी उंगलियों में काफ़ी दर्द था। फिर भी कपड़े पहनने, दाढ़ी बनाने, खाना खाने और दूसरे कई काम करने में उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी लेकिन उन्होंने उसका कोई बावेला नहीं मचाया। चाय पीते समय जब वो बाएं हाथ से चाय का प्याला पकड़े हुए थोड़ी असुविधा में नजऱ आ रहे थे तो किसी ने पूछ लिया, ‘आपकी उंगलियाँ अब कैसी हैं? नेहरू का जवाब था, ‘चिंता की कोई बात नहीं। जल्द ही ठीक हो जाएंगी।’
नेहरू का ग़ुस्सा
नेहरू के व्यवहार में ऊँचे दर्जे की शालीनता थी। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद वो अपने विरोधियों से सामान्य शिष्ट व्यवहार करना नहीं भूलते थे। साल1942 में उनके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से मतभेद हो गए थे क्योंकि राजाजी ने भारत में मुसलमानों के लिए आत्म निर्णय के सिद्धांत को मान लिया था। इस कारण वो देश में एक बड़े तबक़े में अलोकप्रिय हो गए थे।
अप्रैल, 1942 में कांग्रेस कार्यसमिति की इलाहाबाद में बैठक हुई और राजगोपालाचारी उसमें भाग लेने के लिए वहाँ गए। हिंदू महासभा के कुछ समर्थक काले झंडों के साथ रेलवे स्टेशन पर जमा हो गए।
पीडी टंडन लिखते हैं, ‘बहुत व्यस्त होते हुए भी वो राजाजी को स्टेशन लेने जाने वाली कार में बैठ गए। उन्होंने कहा, देखते हैं इलाहाबाद में राजगोपालाचारी को कौन काले झंडे दिखाता है। जैसे ही नेहरू ने काले झंडे लिए प्रदर्शनकारियों को देखा, उन्होंने लपककर उनके हाथ से काले झंडे छीन लिए और उन्हीं के डंडों से उनमें से कुछ को खदेड़ा। प्रदर्शनकारियों का मुखिया जब नेहरू के सामने आया तो वो उस पर चिल्ला पड़े, 'तुम्हारी ये हिम्मत कि इलाहाबाद में मेरे मेहमान की बेइज़्ज़ती करो। हिंदू महासभा के नेता जवाब में कुछ बोले तो वहाँ मौजूद कुलियों को लगा कि वे नेहरू का अपमान कर रहे हैं। वे बेक़ाबू हो गए और उन पर हमला कर दिया। इस पर नेहरू बहुत दुखी हुए, वे अपने हाथों से ढाल बनाकर विरोधी नेता को बचाने लगे।’
निजी सुरक्षा में विश्वास नहीं
नेहरू को सादा भोजन करना पसंद था। 18 जून, 1956 को उनके भोजन के बारे में एक सरकारी नोट जारी किया गया था। उसमें लिखा था, ‘प्रधानमंत्री का आग्रह है कि उनके भोजन के लिए कोई विशेष या अलग तरह का इंतज़ाम न किया जाए।
वो जिस जगह भी होंगे वहाँ का सामान्य भोजन लेना पसंद करेंगे। वो मसाले-मिर्ची खाने के बिल्कुल अभ्यस्त नहीं हैं। वो माँस खाते हैं लेकिन उन्हें सामान्यत: शाकाहारी भोजन ही पसंद है। सुबह वो कॉफ़ी और तीसरे पहर फीकी चाय का एक प्याला लेते हैं।’
गाँधीजी की हत्या के बाद भी नेहरू को अपनी सुरक्षा की कोई खास परवाह नहीं थी। उनकी कार के आगे अंगरक्षकों की कारों का काफि़ला नहीं, बल्कि सिर्फ एक मोटरसाइकिल सवार चला करता था। (bbc.com/hindi)
(बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.)



.jpg)
.jpg)