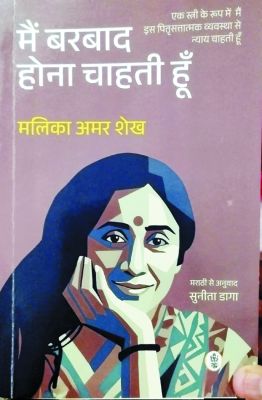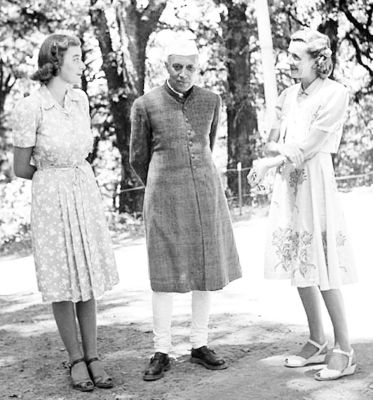विचार / लेख
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) के हालिया आंकड़ों के मुताबिक़, भारत जापान को पीछे छोडक़र दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने की ओर है। इस ख़बर के बाद देशभर में इसकी चर्चा तेज हो गई है।
एक ओर कुछ लोग इसे केंद्र सरकार की नीतियों- जैसे ‘डिजिटल इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’ और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर का परिणाम मानते हैं। उनका कहना है कि इन पहलों ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई है और साथ ही किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के लिए उम्मीदें जगाई हैं।
वहीं दूसरी ओर, कुछ आलोचक इस विकास को सतही मानते हैं। उनका तर्क है कि जब तक हर नागरिक को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलतीं, तब तक भारत विकसित देशों के बराबर नहीं हो सकता।
इन आंकड़ों पर कई सवाल उठते हैं, जैसे- भारत के इस मुकाम तक पहुंचने में मोदी सरकार की किन नीतियों की मुख्य भूमिका रही?
सवाल ये भी है कि अर्थव्यवस्था के तेजी से बढऩे के बावजूद बेरोजगारी दर अब भी ऊँची क्यों है? इस विकास का असली लाभ किन तबकों को मिल रहा है? डिजिटल क्रांति ने इस बदलाव में कैसी भूमिका निभाई?
अगर सब कुछ इतना बेहतर है, तो फिर अमीर-गरीब के बीच की खाई क्यों बढ़ रही है? और सबसे अहम सवाल- इस आर्थिक प्रगति का आम नागरिक की जिंदगी पर असल असर क्या पड़ा है?
इन सवालों पर चर्चा के लिए ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट गौतम चिकरमाने और आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर और अर्थशास्त्री रीतिका खेड़ा शामिल हुए।
आम लोगों की जिंदगी कितनी बदली?
पिछले शनिवार को नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने एक बयान जारी कर भारत के जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा किया।
इस घोषणा के बाद जहां कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसकी सराहना की, वहीं कई विशेषज्ञों ने इस दावे पर सवाल भी उठाए। हर बार जब इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं, तो आम लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि क्या इस आर्थिक तरक्की का असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ा है।
इस सवाल पर आईआईटी दिल्ली की प्रोफेसर और अर्थशास्त्री रीतिका खेड़ा ने कहा, ‘अगर एक परिवार में एक व्यक्ति पांच लाख रुपये कमा रहा है और दूसरे परिवार में चार लोग मिलकर पांच लाख कमा रहे हैं, तो सिफऱ् आमदनी देखकर यह कहना कि दोनों बराबर हैं, ग़लत होगा। क्योंकि एक परिवार में उस राशि से एक व्यक्ति का ख़र्च चल रहा है, जबकि दूसरे में चार लोगों का।’
‘इसी तरह, देशों की तुलना करते समय भी केवल जीडीपी के आंकड़ों से निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। जापान और जर्मनी जैसे देशों की जीडीपी की तुलना भारत से करना उचित नहीं है, क्योंकि भारत की जनसंख्या कहीं ज़्यादा है।’
उन्होंने बताया कि यह जरूर है कि अगर देश में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं तो उम्मीद की जाती है कि इसका फायदा सभी वर्गों तक पहुंचेगा। लेकिन इसके दो अहम पहलू हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने पहलुओं को समझाते हुए कहा, ‘पहला सवाल यह है कि आर्थिक गतिविधि किस सेक्टर में हो रही है? अगर निर्माण क्षेत्र (कंस्ट्रक्शन) में विकास हो रहा है, तो निर्माण मजदूरों तक इसका सीधा लाभ पहुंच सकता है। लेकिन अगर यह वृद्धि फाइनेंशियल सेक्टर में हो रही है, तो इसका लाभ सीमित लोगों तक ही रहेगा- और वो पहले से ही ठीक वर्ग के लोग हैं।’
प्रोफेसर और अर्थशास्त्री रीतिका खेड़ा ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि देश किन क्षेत्रों में निवेश और विकास पर जोर दे रहा है। कौन-से सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं और उनका बाकी अर्थव्यवस्था के साथ कितना गहरा जुड़ाव है।
रीतिका खेड़ा ने कहा, ‘जब हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करते हैं, तो हमें यह सेक्टर-वाइज देखना चाहिए- जैसे कृषि में कितनी वृद्धि हुई, मैन्युफैक्चरिंग में कितना विकास हुआ। इससे यह साफ होता है कि क्या यह आर्थिक प्रगति सभी तक समान रूप से पहुंच रही है या केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही सिमट कर रह गई है।’
लेकिन ऑब्जर्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट गौतम चिकरमाने का मानना है कि हर अर्थव्यवस्था में कुछ वर्ग असंतुष्ट हो सकते हैं।
गौतम चिकरमाने ने कहा, ‘मुझे समझ नहीं आता कि ये आलोचना आ कहां से रही है। ऐसा कौन-सा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसे आर्थिक विकास का लाभ नहीं मिला? मुझे एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं दिख रहा जिसका इससे कोई फ़ायदा न हुआ हो- चाहे वो कृषि हो, मैन्युफैक्चरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप या न्यूनतम वेतन। हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में फ़ायदा हुआ है।’
उन्होंने कहा, ‘हर अर्थव्यवस्था में कुछ वर्ग असंतुष्ट हो सकते हैं, और लोकतंत्र में तो ये आवाज़ें उठना स्वाभाविक भी है।’
आलोचना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, ‘मुझे ये भी समझ नहीं आता कि लोग किस डेटा के आधार पर कह रहे हैं कि असमानता बढ़ गई है, अमीर और अमीर हो गए हैं, और गऱीब वहीं के वहीं हैं।’
सरकारी आंकड़ों पर सवाल क्यों?
चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के इन दावों के बीच कुछ लोगों का कहना है कि भारत एक विशाल आबादी के साथ आर्थिक रूप से सही दिशा में प्रगति कर रहा है जबकि कुछ अर्थशास्त्रियों ने जीडीपी के बारे में दावा करने में जल्दबाजी करने की ओर इशारा किया है।
सरकार जब भी कोई आर्थिक आंकड़ा जारी करती है, तो उस पर अक्सर सवाल उठते हैं। लेकिन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट गौतम चिकरमाने का मानना है कि इतने बड़े स्तर पर आंकड़े केवल सरकार ही जुटा सकती है, और उन्हीं पर भरोसा किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘दुनिया भर में एक ही डेटा प्वाइंट होता है, और वो डेटा सरकारें ही इक_ा करती हैं। किसी और के पास इतनी क्षमता नहीं है। अगर आप कहें कि सरकार ग़लत है, वर्ल्ड बैंक ग़लत है, आईएमएफ़ ग़लत है, एडीबी (एशियन डेवलपमेंट बैंक) ग़लत है, यूनाइटेड नेशंस भी ग़लत है- तो फिर सही कौन है? ये मुझे बता दीजिए, मैं उन आंकड़ों से बहस करने को तैयार हूं।’
इस मुद्दे पर रीतिका खेड़ा ने कहा कि सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठाना कोई नई या गलत बात नहीं है।
उन्होंने समझाया, ‘मान लीजिए किसी देश में केवल दो लोग हैं- एक की आय एक लाख है और दूसरे की चार लाख। ऐसे में कुल जीडीपी पांच लाख हो गई और औसतन प्रति व्यक्ति आय 2।5 लाख हो गई। लेकिन इससे असल आर्थिक स्थिति नहीं समझी जा सकती। अगर सरकार अमीर व्यक्ति से दो लाख लेकर गऱीब को दे दे, तो कुल जीडीपी तो वही रहेगी, लेकिन गऱीब की हालत बेहतर हो जाएगी।’
उन्होंने कहा कि यही वजह है कि ‘हमें आय के वितरण पर ध्यान देना चाहिए। अगर अमीरों से लेकर गऱीबों को दिया जाए, तो असमानता के मुद्दे काफ़ी हद तक सुलझ सकते हैं।’
सरकारी आंकड़ों को लेकर उन्होंने कहा, ‘जीडीपी के आंकड़े कैसे कैलकुलेट होते हैं, उस पर लंबे समय से विवाद होते आए हैं। मेरे हिसाब से हमें सरकारी आंकड़े जरूर देखने चाहिए, लेकिन उन पर सवाल उठाना भी जरूरी है और यह बिल्कुल जायज़ है।’
उन्होंने कहा, ‘जहां तक भारत के जीडीपी रैंक की बात है, मुझे फिलहाल उस आंकड़े पर कोई खास शक नहीं है, लेकिन मैं मानती हूं कि यह सही पैमाना नहीं है। अगर हमें किसी चीज़ से तुलना करनी है, तो वह प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए, न कि कुल जीडीपी।’
बेरोजगारी और सरकारी नौकरी
भारत में बेरोजगारी एक गंभीर और जटिल समस्या है, जो खासतौर पर युवाओं, महिलाओं और शिक्षित वर्ग को प्रभावित करती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कई लोग सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा में समय गंवा देते हैं, जबकि अन्य का कहना है कि देश में पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं हैं, जिससे लोग बेरोजगार रह जाते हैं।
देश में जब भी चुनाव होते हैं, विपक्षी पार्टियां बेरोजग़ारी के मुद्दे को हथियार बनाकर सरकार पर निशाना साधती हैं। इस पर अर्थशास्त्री रीतिका खेड़ा ने कहा, ‘बहुत सारे लोग पूरी तरह से बेकार नहीं बैठ सकते, इसलिए बेरोजग़ारी की दर हमेशा बहुत ज़्यादा नहीं दिखती। जिन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती, वे कुछ न कुछ काम करने लगते हैं- जैसे साइकल मरम्मत की दुकान खोल लेना। इस तरह लोग किसी तरह अपना गुज़ारा करने की कोशिश करते हैं।’
गिग इकॉनमी पर बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘गिग वर्क में आमदनी ज़्यादा नहीं होती। कभी-कभार सुनने में आता है कि किसी ने बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन वो अपवाद होता है। अगर औसत देखें तो कमाई बहुत सीमित है।’
सरकारी नौकरी को लेकर उन्होंने कहा, ‘ऐसा नहीं है कि हर सरकारी नौकरी में तनख्वाह बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसमें जॉब सिक्योरिटी और दूसरी सुविधाएं होती हैं, जो लोगों को आकर्षित करती हैं।’
साथ ही उनका मानना है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में भी धीरे-धीरे वही फ़ायदे मिलने लगें- जैसे सुरक्षा, स्थायित्व, और सम्मान- तो लोग उस तरफ़ भी बढऩे लगेंगे।
रीतिका खेड़ा ने कहा, ‘एक बहुत बड़े तबके के लिए मज़दूरी की दरें या तनख्वाएं बहुत कम हैं और वहां नौकरी की सुरक्षा भी नहीं होती। कभी भी निकाल दिया जाता है। इस वजह से भी लोग उस सेक्टर से कतराते हैं।’
उन्होंने कहा, ‘हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका है जो रोजी-रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। अलवर में एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि ‘मिडिल क्लास वो है जो अगर आज रोजग़ार मिल गया तो शाम को रोटी के साथ सब्जी खा पाएगा और अगर नहीं मिला तो सिर्फ सूखी रोटी खाएगा’।’
बेरोजगारी को लेकर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट गौतम चिकरमाने अलग विचार रखते हैं। उनका मानना है कि देश में बेरोजग़ारी उतनी ज़्यादा नहीं है।
उन्होंने कहा कि समस्या ये है कि ज़्यादातर युवाओं के लिए नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी है। अगर नजरिया यही रहेगा, तो फिर नौकरियाँ सीमित होंगी और उतनी होनी भी नहीं चाहिए।
उन्होंने आगे कहा, ‘अगर कोई युवक 20-25 साल की उम्र से लेकर 30-35 साल की उम्र तक सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी करता रहे और फिर कहे कि वो बेरोजगार है, तो इसमें न आप कुछ कर सकते हैं, न मैं और न ही सरकार।’
कैसे बेहतर हो सकते हैं हालात?
इस सवाल पर गौतम चिकरमाने का मानना है कि हर समस्या का समाधान आर्थिक विकास में ही है।
उन्होंने कहा, ‘अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो मज़दूरों को रोजग़ार मिलेगा। सबसे अहम बात यह है कि कृषि से मैन्युफैक्चरिंग और फिर मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस सेक्टर तक जो बदलाव होना है, वो भी इसी ग्रोथ से संभव होगा।’
एक अनुभव शेयर करते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं उत्तराखंड में किसानों के साथ काम करने गया था। वहां देखा कि किसानों को खेत के लिए मज़दूर नहीं मिल रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग नरेगा में सडक़ निर्माण में लगे हुए हैं।’
उन्होंने कहा, ‘हमारा कृषि क्षेत्र बेहद अनुत्पादक (कम उत्पादक) है। हमें इसकी उत्पादकता दस गुना बढ़ानी होगी, जो केवल श्रमिकों के जरिए नहीं बल्कि मैकेनाइजेशन (मशीनीकरण) से संभव है।’
उन्होंने कहा, ‘इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे रिफॉर्म लाएं जिससे प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में निवेश के लिए प्रेरित हो।’
चिकरमाने ने कहा, ‘मुझे लगता है कि मौजूदा ग्रोथ की रफ़्तार बनी रहनी चाहिए।’ (bbc.com/hindi)