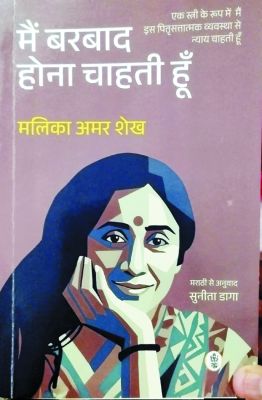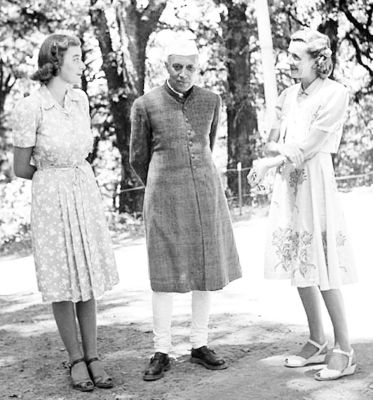विचार / लेख
- नित्या पांडियन
‘दोपहर का समय था। मेरी मां, मैं और मेरी बहन पिता के आने का इंतजार कर रहे थे। उस दिन रविवार था और घर में नॉन वेज बना था। लेकिन पापा के आने में देर हो गई। मां ने मुझे और बहन को खाना खिला दिया और खुद उनके आने का इंतज़ार करती रहीं। उस दिन दोनों ने शाम के पाँच बजे दोपहर का खाना खाया।’
‘पिछले 30 सालों में, मेरी मां ने शायद हर दिन इसी तरह से अपना खाना खाया होगा। मुझे याद नहीं कि कभी उन्होंने हमारे साथ बैठकर खाना खाया हो।’
चेन्नई में रहने वाले प्रशांत बीबीसी से अपनी बात कुछ ऐसे कहते हैं।
मैंने घरों में महिलाओं के खाने के तौर-तरीकों पर जहां भी बात की, ज़्यादातर जगहों पर यही स्थिति देखने को मिली।
खाना, यानी महिलाएं जो खाती हैं, एक ऐसी गतिविधि है जिस पर बहुत कम बात होती है।
लेकिन बहु-सांस्कृतिक भारतीय समाज में महिलाओं के खाने को लेकर चर्चा आखऱि कब होती है?
क्या कभी महिलाओं के स्वास्थ्य को गंभीरता से लिया जाता है?
खाने की राजनीति में महिलाओं के हिस्से के खाने को किस नजऱ से देखा जाता है?
क्या हमारे खाने की संस्कृति में भी पितृसत्तात्मक सोच गहराई से शामिल है?
परंपरा के तौर पर अपनाना
बीबीसी से कई महिलाओं ने कहा, ‘महिला को अक्सर त्याग की देवी के तौर पर दर्शाया जाता है। कई मौकों पर महिलाओं से ये अपेक्षा की जाती है कि वह ख़ुद से ऊपर परिवार नामक संस्था को रखे। यह अपेक्षा महिलाओं से पीढिय़ों से रखी जा रही है।’
चेन्नई में रहने वाली आनंदी ने बीबीसी से बात करते हुए उस सलाह को याद किया जो उनकी मां ने उन्हें शादी के दौरान दी थी। उस समय आनंदी 21 साल की थीं।
आनंदी बताती हैं, ‘मां खुद के लिए कुछ नहीं पकाती हैं। सबके खाने के बाद जो कुछ खाना बचता था, वो वही खाना खा लेती थीं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहती हूं कि तुम भी ऐसी ही बनो।’
आनंदी ने कहा, ‘मुझे नहीं पता कि मेरी मां और दादी ने कभी अपनी पसंद का खाना पकाया या नहीं। लेकिन उन्होंने हमेशा सबके खाने के बाद ही खाना खाया होगा।’
सत्या एक किसान परिवार से आती हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया, ‘जब मेरी शादी हुई तो एक दिन दोपहर में मुझे भूख लग रही थी, मैंने खुद के लिए खाना बनाकर खा लिया। इसके बाद जब शाम को मेरी सास आईं तो उन्होंने कहा कि क्या चार बजे किसान के घर खाना बना कर खाने से परिवार में समृद्धि आएगी।’
‘उसके बाद से मैंने शाम को खाना खाना पूरी तरह से बंद कर दिया। भले ही मुझे कितनी भी भूख क्यों न लगी हो।’
क्या ये चलन हर जगह है?
बीबीसी से कई महिलाओं ने अपने अनुभवों को साझा किया।
एक महिला ने कहा, ‘हमारे घर में पुरुषों को जब खाना दिया जाता है तो उन्हें खाना अच्छे तरीके से भरपूर सब्जियों के साथ परोसा जाता है जबकि महिलाओं की थाली में बचा हुआ खाना ही आता है।’
‘नॉन वेज खाने में से भी मीट का सबसे अच्छा हिस्सा हमेशा पुरुषों को ही परोसा जाता है।’
उन्होंने कहा, ‘अगर हमारे घर में पिता और भाई नहीं होते हैं तो हमारे घर में उस दिन नॉन वेज खाना नहीं बनता है।’
सुमैया मुस्तफा एक ऐसे तमिल मुस्लिम परिवार से आती हैं जहां समाज मातृ-सत्तात्मक व्यवस्था में जीता है।
वह कहती हैं, ‘अन्य समुदायों की तुलना में यहां भोजन की राजनीति थोड़ी अलग है। हमारे इलाके़ में शादी के बाद पुरुषों के अपनी पत्नी के घर आकर रहने की परंपरा है। चूंकि महिलाएं घर की मुखिया होती हैं, इसलिए उन्हें पुरुषों की तुलना में अधिक सुविधाएं और विशेषाधिकार मिलते हैं।’
सुमैया एक लेखिका हैं जो भारत के तटीय शहरों में रहने वाले छोटे जातीय समूहों की संस्कृति और भोजन पर रिसर्च कर रही हैं। वे थुथुकुडी जिले के कयालपट्टिनम की मूल निवासी हैं।
महिलाओं के भोजन पर कब ध्यान दिया जाता है?
केवल पहली बार पीरियड्स होने पर और पहली प्रेग्नेंसी के दौरान ही महिलाओं के खान-पान को लेकर ज़्यादा चिंता जताई जाती है।
सुमैया कहती हैं, ‘हमें समझना चाहिए कि ये दोनों मौके दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने के तरीके़ हैं। ये सिर्फ महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़े नहीं हैं। हम ऐसी सोच इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारे समाज में बच्चे के जन्म को बहुत अहमियत दी जाती है।’
उन्होंने कहा, ‘हमारा समाज कई धर्मों और संस्कृतियों से मिलकर बना है, लेकिन जब बात खाने और महिलाओं की होती है, तो अलग-अलग समूहों में भी एक जैसी ही सोच दिखाई देती है।’
इन खास मौकों (जैसे पीरियड्स और बच्चे के जन्म) के अलावा भी, महिलाओं के शरीर में एक और बड़ा बदलाव आता है वो है मेनोपॉज। इस दौरान उन्हें अच्छे और पोषक आहार की जरूरत होती है।
कृषि और महिलाओं के जीवन पर लिखने वाली अपर्णा कार्तिकेयन कहती हैं, ‘इस बारे (मेनोपॉज) में ज़्यादा बात नहीं की जाती।’
अपर्णा बताती हैं, ‘मेनोपॉज के समय महिलाओं की सेहत, उनके खाने और मानसिक स्थिति के बारे में कोई ज़्यादा परवाह नहीं करता है। यह तक नहीं सोचा जाता कि उन्हें किस तरह का खाना चाहिए। अब लोग पहले से ज़्यादा उम्र तक जी रहे हैं, लेकिन समाज ऐसा बर्ताव करता है जैसे पीरियड्स खत्म होने के बाद महिलाओं की जि़ंदगी भी खत्म हो जाती है।’
वो कहती हैं, ‘कोई हमें नहीं बताता कि पीरियड्स के दौरान क्या खाना चाहिए। मुझसे पहले की पीढ़ी की महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक नहीं थीं। मुझे भी 45 साल की उम्र के बाद ही इसके बारे में जानकारी मिली। मेरी अपनी ही उम्र की दूसरी महिलाओं से भी इस पर कोई बातचीत नहीं होती थी। हमारे समाज ने हमें ऐसा बना दिया है कि हम यह मान ही नहीं पाते कि अच्छा खाना महिलाओं के जीवन में कितना जरूरी है।’
महिलाओं और खाने के बीच का रिश्ता
वरिष्ठ पत्रकार जया रानी सालों से अनुसूचित जातियों के जीवन पर रिपोर्टिंग कर रही हैं। उन्होंने बीबीसी से बातचीत में गांवों में खाने-पीने और मेहमाननवाजी की परंपरा पर बात की।
वो कहती हैं, ‘अगर किसी घर में मटन करी बनी है, तो आज भी सबसे स्वादिष्ट और पौष्टिक हिस्सा पहले मर्दों और लडक़ों को दिया जाता है। त्योहारों के दौरान जब पकवान बनते हैं तो उन्हें भी पुरुष ही पहले खाते हैं, महिलाएं काम पूरा करके आखिर में खाती हैं।’
जया रानी आगे बताती हैं, ‘महिलाओं का रिश्ता खाने को सिफऱ् पकाने तक होता है। ये सीधा उनकी थाली से नहीं जुड़ता है। हमारे समाज में आमतौर पर सभी लोग एक साथ बैठकर नहीं खाते।’
वो कहती हैं, ‘यहां ज़्यादातर ऐसा होता है कि मर्द बैठकर खाते हैं और औरतें परोसती हैं। आपने शायद ही कभी किसी मर्द को ये कहते सुना होगा, ‘तुमने खाना पकाया है, अब मैं तुम्हारे लिए खाना परोसता हूं’।’
वो आगे कहती हैं, ‘अक्सर मर्द ये बिना देखे खाना खा लेते हैं कि दूसरों के लिए कुछ बचा भी है या नहीं। उन्हें पता होता है कि घर की महिलाएं दही या म_े के साथ सूखा चावल खाकर गुजारा कर लेंगी और वे ये भी जानते हैं कि इसे लेकर महिलाएं कोई शिकायत नहीं करेंगी।’
नाइजीरियाई लेखक चिनुआ अचेबी ने अपनी मशहूर किताब ‘थिंग्स फॉल अपार्ट’ में अफ्रीका की एक जनजाति के उस आदमी के बारे में लिखा है, जिसे अगर उसकी पत्नी समय पर खाना न दे, तो क्या अंजाम भुगतना पड़ता है।
ऐसे साहित्य ये बताते हैं कि महिलाओं और खाने के बीच का रिश्ता सिफऱ् भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत गहरा और जटिल है।
‘जब मैं उसके परिवार के बारे में सोचता हूं, तो मुझे ओवन में पकते हुए मांस की खुशबू, लहसुन और आग की महक, किचन में बर्तनों की आवाज़ें और वहां से आती महिलाओं की आवाजें याद आती हैं।’
‘मेरे चाचा जिंदा मछली को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटते थे। मेरी पत्नी और उसकी बहन मुर्गे को एकदम कसाई की तरह काटती थीं।’
ये पंक्तियां ‘द वेजिटेरियन’ किताब से ली गई हैं, जिसे साल 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली लेखिका हान कांग ने लिखा है।
यहां हान कांग ने दिखाया है कि जब कोई पुरुष अपनी पत्नी और उसके घर के बारे में सोचता है, तो उसके मन में क्या आता है।
इसी तरह फिल्म ‘इंग्लिश विंग्लिश’ में एक सीन है, जहां सतीश (आदिल हुसैन) अपने रिश्तेदारों के बीच अपनी पत्नी के बारे में कहता है, ‘शशि (श्रीदेवी) को अगर कुछ अच्छा लगता है तो बस लड्डू बनाना।’
जया रानी कहती हैं, ‘सच कहें तो आज की फिल्मों में महिलाओं को बहुत ‘शुद्ध’ तरीके से दिखाया जाता है। महिलाएं खाना बनाते हुए तो दिखती हैं, लेकिन खाते हुए कम ही और अगर खाती भी हैं तो खाना शाकाहारी ही होता है।’
वो आगे कहती हैं, ‘जहां घरेलू हिंसा होती है, वहां मां या सास ही बहू के लिए पौष्टिक खाना बनाने की जिम्मेदारी उठाती हैं। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं घरेलू हिंसा के बावजूद परिवार छोडक़र नहीं जातीं, इसलिए उनके लिए खाना एक सहारा बन जाता है।’
आजकल सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनमें महिलाएं अपने पति के लिए खाना बनाती दिखती हैं। भले ही सोशल मीडिया को तरक्की की निशानी माना जाता है, लेकिन आज भी महिलाएं अक्सर अपने लिए वही पारंपरिक, जेंडर-आधारित काम दिखाने को मजबूर होती हैं।
आंकड़े क्या कहते हैं?
सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं को कम खाने और दिन के अंत में खाने की आदत होती है।
विश्व खाद्य कार्यक्रम यूएसए (डब्ल्यूएफ़पीयूएसए) के आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया में खाने की कमी से जूझ रहे 69 करोड़ लोगों में से 60 फीसदी महिलाएं हैं।
डब्ल्यूएफपीयूएसए की आधिकारिक वेबसाइट पर भी कहा गया है, ‘दुनिया के कुछ देशों में, महिलाएं पारंपरिक तौर पर परिवार के पुरुषों और लडक़ों के खाने के बाद ही खाना खाती हैं। महिलाएं ही अक्सर संकट के समय में अपना खाना दूसरों के साथ बांटती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि परिवार के सदस्यों को पूरा खाना मिले।’
साल 2019-2021 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफ़एचएस) के मुताबिक, पुरुषों की तुलना महिलाओं में एनीमिया होने की ज़्यादा आशंका रहती है।
15 से 49 साल की उम्र की जो महिलाएं गर्भवती नहीं हैं, उनमें से 53.2 फीसदी महिलाएं एनीमिया से जूझ रही हैं।
वहीं इसी उम्र वर्ग की 50.4 फीसदी गर्भवती महिलाएं भी एनीमिया की शिकार हैं। दूसरी ओर इसी आयु वर्ग के 22.7 फीसदी पुरुषों में भी एनीमिया पाया गया है।
डॉ. मीनाक्षी बजाज तमिलनाडु सरकार की मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, ओमंदूरार में न्यूट्रिशनिस्ट हैं।
इस बारे में बात करते हुए वह कहती हैं, ‘महिलाओं को किशोरावस्था, गर्भावस्था और स्तनपान के समय ज़्यादा पोषण की जरूरत होती है।’
वह कहती हैं, ‘मेनोपॉज एक ऐसा दौर होता है जिसमें महिलाओं को कैल्शियम, विटामिन डी और फाइबर की कमी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर इस बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है।’ (bbc.com/hindi)