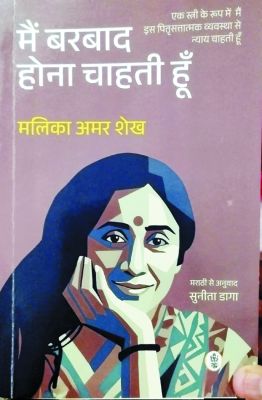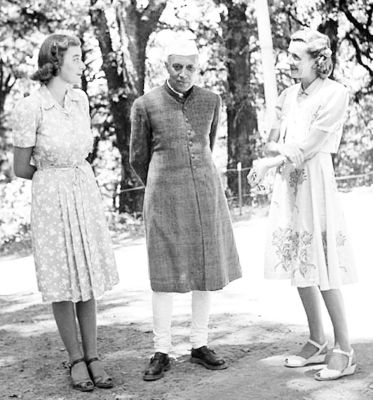विचार / लेख
-सुभोजित बागची
तेलंगाना के वारंगल जि़ले में स्थित कड़वेंदी गांव बाहर से देखने पर एक आम भारतीय गांव जैसा ही लगता है। लेकिन इसे अलग बनाते हैं, वहां सफेद रंग किए गए ईंट-पत्थर के घरों के बीच बने दर्जनों बड़े लाल रंग के समाधि-स्थल। गांव के बीचों-बीच डोड्डी कोमुरैय्या की एक समाधि है, जो कड़वेंदी में जन्मे एक किसान नेता थे।
4 जुलाई 1946 को उनकी हत्या इसी गांव में कर दी गई थी। गांव के बारे में निज़ाम कॉलेज, हैदराबाद में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष और एसिस्टेंट प्रोफेसर रामेश पन्नीरू लिखते हैं, ‘कोमुरैय्या की शहादत ने ही तेलंगाना के सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत की।’
1946 से 1951 के बीच तेलंगाना में हुआ किसान विद्रोह, आगे चलकर भारत में माओवादी आंदोलन की प्रेरणा बना। कोमुरैय्या की शहादत के बाद कड़वेंदी के सैकड़ों लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया और अपनी जान गंवाई। गांव की समाधियों पर खुदे उनके नाम आज भी उनकी ‘कुर्बानी’ की गवाही देते हैं।
अप्रैल की एक गर्म और उमस भरी दोपहर को, राजशेखर अपनी बहन गुमुदावेल्ली रेणुका की याद में बन रही एक नई समाधि का काम देख रहे थे।
रेणुका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की मीडिया प्रभारी थीं और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में इस प्रतिबंधित संगठन की दंडकारण्य विशेष जोनल कमिटी की सदस्य थीं। 31 मार्च को रेणुका की मौत सीपीआई (माओवादी) के खिलाफ चल रहे सुरक्षाबलों के एक ऑपरेशन के दौरान हुई थी।
सरकार ने एलान किया है कि वह मार्च 2026 तक माओवादी आंदोलन को पूरी तरह खत्म कर देगी।
राजशेखर कहते हैं, ‘कोमुरैय्या से लेकर रेणुका तक यह सफऱ 70 सालों का है, जिसमें हर साल कड़वेंदी में एक नई समाधि जुड़ती जाती है।’ लेकिन 21 मई को यह सफर एक नए मोड़ पर आकर रुक-सा गया, जब सीपीआई (माओवादी) के महासचिव नंबाल्ला केशव राव उर्फ बसवराजू छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों से लड़ते हुए मारे गए।
कई लोगों को लगता है कि बसवराजू की मौत के साथ भारत में माओवादी आंदोलन खत्म हो सकता है। या हो सकता है कि यह आंदोलन बस कुछ समय के लिए रुका हो और फिर किसी और रास्ते से दोबारा शुरू हो जाए, जैसा पहले कई बार हुआ है।
भारत में माओवादी आंदोलन
1946 में तेलंगाना में जो सशस्त्र किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उसके लगभग दो दशक बाद, 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी नाम के कस्बे में जमींदारों के खिलाफ एक किसान विद्रोह हुआ। यही आंदोलन धीरे-धीरे भारत में माओवादी विचारधारा की नींव बना।
1970 के दशक में यह माओवादी आंदोलन तेज़ी से फैला और बंगाल, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और आज के छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों तक पहुंच गया।
साल 2004 में सीपीआई (माओवादी) का गठन हुआ। यह पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माक्र्सवादी-लेनिनवादी), पीपुल्स वॉर ग्रुप (जिसे पीडब्ल्यूजी के नाम से जाना जाता था) और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ़ इंडिया (एमसीसीआई) के विलय से बनी।
पिछले कई सालों से माओवादियों की मुख्य गतिविधियां छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके से संचालित हो रही थीं, जो क्षेत्रफल में लगभग केरल राज्य जितना बड़ा है। हाल ही में बस्तर के अंदरूनी हिस्से में माओवादी नेता बसवराजू की मौत हुई। इससे संकेत मिला कि माओवादियों की आखिरी मजबूत पकड़ भी अब टूट चुकी है और यह प्रतिबंधित संगठन अब पूरी तरह ख़त्म होने की कगार पर है।
हालांकि, हैदराबाद में मौजूद सामाजिक विश्लेषक और पत्रकार एन। वेणुगोपाल ऐसा नहीं मानते। माओवादी आंदोलन पर वे एक दर्जन से अधिक किताबें लिख चुके हैं।
वेणुगोपाल कहते हैं, ‘थोड़ी शांति जरूर आएगी, लेकिन पहले भी जब सत्तर के दशक में माओवादी नेताओं की हत्या हुई थी, तब भी आंदोलन नहीं रुका। आज भी हम नक्सलवाद पर बात कर रहे हैं।’
उनका मानना है कि माओवादियों ने दलितों और आदिवासियों के बीच आत्मविश्वास पैदा किया, जातिगत शोषण का विरोध किया और गरीबों में जमीन का बंटवारा सुनिश्चित किया।
वेणुगोपाल कहते हैं, ‘आज भी आप अक्सर टीवी पर लोगों को यह कहते सुनेंगे कि ‘अन्नालु’ (नक्सलियों के लिए प्रचलित शब्द, जिसका मतलब होता है ‘बड़ा भाई’) ने नेताओं की तुलना में ज़्यादा सामाजिक न्याय दिया।’
हैदराबाद के एक मुख्य कारोबारी, जो 1970 के दशक में नक्सलियों के छात्र संगठन रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन (आरएसयू) के नेता थे, वो भी इस सोच से सहमत हैं। नाम न छापने की शर्त पर उन्होंने बताया कि 70 और 80 के दशक में ‘तेलुगु भूमि’ (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) के कई शिक्षित लोग बड़ी संख्या में आरएसयू से जुड़े थे।
उन्होंने कहा, ‘हमारी पीढ़ी के लोग यह कभी नहीं भूलेंगे कि हम अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेज पाए क्योंकि अन्नालु ने उस दौर में छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया, जब सरकार तीन दशकों तक नाकाम रही थी।’
हालांकि 1980 के दशक के मध्य तक तेलंगाना में माओवादी हिंसा को काफी हद तक रोक दिया गया। सरकार ने दोहरी रणनीति अपनाई, एक ओर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया तो दूसरी ओर, पिछड़े इलाकों के लिए विशेष कल्याण योजनाएं शुरू कीं। इनमें स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता जैसे कार्यक्रम शामिल थे।
साल 2016 में एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने हमें बताया था कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास की योजना ने विशेष रूप से अहम भूमिका निभाई। बाद में यही रणनीति छत्तीसगढ़ में भी अपनाई गई।
माओवाद : तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़ तक
चंबला रविंदर पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के सैन्य कमांडर रह चुके हैं। साल 2010 में, जब वे बस्तर में पार्टी की उत्तरी इकाई के प्रमुख थे, तो उन्होंने बीबीसी को बताया था कि 70 और 80 के दशक में माओवादी गुट, पीडब्ल्यूजी ने कई अच्छे काम किए थे, ‘लेकिन जब सरकार की सख्त कार्रवाई शुरू हुई, तो वे उस काम को बचा नहीं पाए।’
उन्होंने बताया कि इस अनुभव से सबक लेते हुए माओवादियों ने छत्तीसगढ़ में अपनी रणनीति बदली।
15 साल पहले उन्होंने बीबीसी से कहा था, ‘बस्तर में हमने शुरुआत से ही सैन्य संगठन बनाने पर जोर दिया।’
रविंदर ने साल 2014 में आत्मसमर्पण कर दिया और अब हैदराबाद के एक कॉलेज में सुरक्षा प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं।
पिछले हफ्ते उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, ‘न तो तेलंगाना में किया गया सामाजिक काम टिक पाया और न ही छत्तीसगढ़ में जंगलों के लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई गुरिल्ला सेना कारगर साबित हुई।’
लेकिन एन। वेणुगोपाल बताते हैं कि कुछ वजहों से माओवादी बीते सालों में छत्तीसगढ़ में एक बड़ी ताकत बन गए।
छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है।
इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स की साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक, यह राज्य टिन कंसन्ट्रेट और मोल्डिंग सैंड का इकलौता उत्पादक है। साथ ही ये कोयला, डोलोमाइट, बॉक्साइट और अच्छी गुणवत्ता वाले लौह अयस्क का भी प्रमुख उत्पादक है।
वेणुगोपाल का मानना है कि माओवादियों की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि उन्होंने खनन कंपनियों को इन संसाधनों तक पहुंचने से रोके रखा।
वे कहते हैं, ‘माओवादियों ने ‘जल, जंगल, ज़मीन’ के सिद्धांत पर आंदोलन खड़ा किया। इस सोच के साथ कि जंगल और जमीन आदिवासियों की है, मल्टीनेशनल कंपनियों की नहीं। इसी वजह से अब तक कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन इलाकों में घुस नहीं सकीं।’
छत्तीसगढ़ में माओवादियों का पतन
हाल ही में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षाबलों की कार्रवाई जिसमें बसवराजू की मौत सबसे अहम घटना रही, ऐसे वक्त में हुई है जब गृह मंत्रालय ने अपनी पिछली रिपोर्ट (2023-24) में बताया था कि ‘केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती, इंडिया रिजर्व बटालियन की मंजूरी, राज्य पुलिस बलों को बेहतर बनाने और आधुनिक सुविधाएं देने, सुरक्षा से जुड़ी लागत की भरपाई, राज्यों की विशेष खुफिया शाखाओं और विशेष दस्तों को मजबूत करने की कोशिश की गई।’
इसमें कहा गया है, ‘पुलिस थानों को बेहतर तरीके से तैयार करने , माओवादी इलाकों में ऑपरेशन के लिए हेलिकॉप्टर की सुविधा देने, राज्य पुलिस को प्रशिक्षण में मदद करने, खुफिया सूचनाएं साझा करने, राज्यों के बीच तालमेल बढ़ाने और स्थानीय लोगों से जुड़ाव बढ़ाने जैसे कदम उठाए गए थे।’
ये सारे कदम नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान टू एड्रेस एलडब्ल्यूई के तहत उठाए गए थे, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में मंज़ूरी दी थी।
गृह मंत्रालय में एलडब्ल्यूई विभाग के पूर्व संयुक्त सचिव एम। ए। गणपति ने कहा, ‘इस नीति की वजह से छत्तीसगढ़ पुलिस ने ‘बहुत सटीक हमले करने’ की क्षमता विकसित कर ली है।’
गणपति, जिन्होंने नक्सलियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार किया था, बताते हैं, ‘केंद्रीय अर्धसैनिक बल पुलिस कैंप स्थापित करने, जमीन पर मौजूदगी बनाए रखने और राज्य पुलिस के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने जैसे होल्डिंग ऑपरेशन करते रहे। इस दौरान राज्य पुलिस ने खुफिया सूचनाएं जुटाईं और विशेष बलों ने अभियान चलाए।’
उन्होंने कहा ‘ऑपरेशन के दौरान अर्धसैनिक बलों ने घेराबंदी की, ताकि माओवादी भाग न सकें। ये जिम्मेदारियों का साफ बंटवारा और अच्छा समन्वय था।’
दक्षिण छत्तीसगढ़ के पत्रकार कमल शुक्ला, जो कई वर्षों से इस संघर्ष को करीब से देख रहे हैं, बताते हैं कि राज्य पुलिस की नक्सल विरोधी इकाई, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स (डीआरएफ) में पूर्व नक्सलियों की भर्ती से पुलिस की लड़ाकू क्षमता में बढ़ोतरी हुई है।
उन्होंने कहा, ‘सरेंडर किए हुए नक्सली इलाके को अच्छी तरह जानते थे और छिपने की जगहों की पहचान कर सकते थे। साथ ही उन्हें विद्रोहियों की ताकत और कमजोरियों की भी बेहतर समझ थी, जिससे पुलिस को काफ़ी मदद मिली।’
माओवादियों ने भी 25 मई को जारी अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति में माना कि जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, उनमें से कुछ ने बसवराजू के मारे जाने में अहम भूमिका निभाई।
बयान में कहा गया, ‘पिछले छह महीनों में, माड़ (अबूझमाड़) क्षेत्र के कुछ सदस्य कमजोर पड़ गए और उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वे गद्दार बन गए।’
हालांकि, अर्द्धसैनिक बलों ने भी मोर्चा संभाला और हेलिकॉप्टर से अभियान जारी रहा।
शुक्ला ने बताया, ‘हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में ड्रोन तैनात किए गए, जो इस अभियान का एक नया पहलू था।’
माओवाद से निपटने की नेशनल पॉलिसी के तहत, केंद्र सरकार की एजेंसियों को हेलिकॉप्टर संचालन और नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा कैंपों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 765 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय में पूर्व अधिकारी और नक्सल विरोधी अभियानों के विशेषज्ञ एम। ए। गणपति का कहना है कि अब माओवादी विचारधारा नई पीढ़ी को आकर्षित नहीं कर पा रही है, इसी वजह से उनके संगठन से जुडऩे वाले लोगों की संख्या लगातार घटती गई है।
उन्होंने बताया कि माओवादी जनता की बदलती सोच और जरूरतों को समझने में असफल रहे।
गणपति का कहना है, ‘जब मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का दौर आया, तो लोग बाहरी दुनिया से जुडऩे लगे। ऐसे हालात में आप जंगल के किसी कोने में बैठकर, समाज से कटकर ज़्यादा समय तक सक्रिय नहीं रह सकते। माओवादी भी अब नई सामाजिक सच्चाइयों से कटे हुए रहकर, छिपकर काम नहीं कर सकते।’
इसके अलावा, केंद्र सरकार ने ‘सडक़ और टेलीकॉम कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी ढांचे को सुधारने और स्थानीय लोगों के कौशल विकास के लिए विशेष योजनाएं शुरू कीं।’ यह बात 2023-24 की रिपोर्ट में दर्ज है।
एक पूर्व नक्सली नेता, जो 1980 के दशक में बिहार में सक्रिय थे, उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि छत्तीसगढ़ में हिंसा कहीं ज़्यादा भीषण रही, क्योंकि वहां माओवादियों की सैन्य ताकत तेलंगाना की तुलना में कहीं अधिक थी।
उन्होंने कहा, ‘तेलंगाना में माओवादी कई स्क्वॉड, प्लाटून, कंपनी और बटालियन गठित करने में कामयाब रहे। जबकि बंगाल, बिहार और तेलंगाना के कुछ इलाकों में वो केवल स्क्वॉड तक ही सीमित रह गए। बिहार में कुछ गुरिल्ला प्लाटून जरूर बने थे, लेकिन वे भी पारंपरिक सेना के मुकाबले काफी छोटे थे।’
इन प्रयासों और रणनीतिक बदलावों का असर यह हुआ कि गृह मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, 2013 के मुकाबले 2023 में माओवादी हिंसा की घटनाओं में 48 फीसदी की गिरावट आई (1136 से घटकर 594 मामले), और इस हिंसा में नागरिकों और सुरक्षाबलों की मौतों की संख्या 65 फीसदी घटी (397 से घटकर 138 मौतें)।
सियासी नाकामी
माओवादी आंदोलन को करीब से देखने वाले विशेषज्ञों का कहना हैं कि सुरक्षाबलों ने माओवादियों को कमजोर करने में बाहरी तौर पर भूमिका निभाई, संगठन के भीतर की राजनीतिक नाकामियों ने उन्हें अंदर से कमज़ोर किया।
2007 में सीपीआई (माओवादी) ने अपने राजनीतिक दस्तावेज में कहा था कि वे सरकार से आजाद ‘स्वतंत्र क्षेत्र’ बनाएंगे और इन इलाकों से लंबा ‘जनयुद्ध’चलाकर ‘क्रांति’ लाएंगे। ये दस्तावेज साल 2004 में तैयार किया गया था।
ये सोच चीन के नेता माओ त्से तुंग से प्रेरित थी, जिन्होंने लगभग सौ साल पहले चीन में इसी तरीके से क्रांति की थी।
सीपीआई (माओवादी) के एक पूर्व समर्थक ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि यह मॉडल आज के समय में काम नहीं कर सकता।
उन्होंने कहा, ‘माओवादियों का सपना था कि वे ऐसे इलाकों में अपना दबदबा बनाएंगे जहां सरकार की पकड़ कमजोर हो। लेकिन जैसे ही सरकार ने सख्ती से कार्रवाई की, ये आधार क्षेत्र खत्म हो गए और भारी जान-माल का नुकसान हुआ।’
उन्होंने यह भी कहा कि माओवादियों को सोचना होगा कि क्या अब भी जंगलों में रहकर कोई क्रांति लाई जा सकती है या इसी वजह से वे जनता से दूर होते चले गए।
उन्होंने आगे कहा, ‘अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो भी वे असफल क्यों हुए, यह सवाल उठता है। मेरी समझ में, चाहे वह तेलंगाना में सामाजिक न्याय देने की कोशिश हो या छत्तीसगढ़ में सैन्य ताकत के बल पर आदिवासियों को एकजुट करना, माओवादी इन दोनों को एक राजनीतिक ताकत में नहीं बदल पाए।’
वेणुगोपाल ने भी माना कि ‘स्वतंत्र क्षेत्र’ की सोच पर अब दोबारा विचार किए जाने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं होगा।
उनका मानना है कि ‘चाहे कितने भी नेता मारे जाएं, लोगों की उम्मीदें नया नेता तलाश लेंगी। जब तक सामाजिक अन्याय रहेगा, तब तक कोई न कोई नेता और आंदोलन जरूर होगा। भले ही वो माओवादी आंदोलन न हो।’
क्या यही माओवादी आंदोलन का अंत है?
बसवराजू की मौत को लेकर कई लोगों का मानना है कि भारत में माओवादी आंदोलन अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है।
नक्सल विरोधी अभियानों के विशेषज्ञ एम। ए। गणपति का कहना है कि मौजूदा हालात में माओवादियों के पास पलटकर लडऩे का कोई वास्तविक मौका नहीं है।
उन्होंने कहा, ‘यह समय सरकार से बातचीत करने का है, न कि बिना वजह अपने कैडर की बलि देने का। हालांकि मैं सरकार की ओर से कुछ नहीं कह सकता।’
माओवादी अप्रैल से ही बिना शर्त संघर्ष विराम और शांति वार्ता की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अब तक कम से कम तीन बयान जारी किए हैं, जिनमें से एक 25 मई को जारी किया गया था।
बसवराजू के ख़िलाफ़ चले ऑपरेशन के बाद उन्होंने एकतरफ़ा संघर्ष विराम का ऐलान किया। साथ ही अफ़सोस जताया कि सरकार ने शांति वार्ता शुरू करने के लिए नागरिक समाज की अपीलों पर ध्यान नहीं दिया।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, जहां माओवादियों को अब भी कुछ हद तक ज़मीनी समर्थन हासिल है, सिविल सोसाइटी के कई कार्यकर्ता संघर्ष विराम और बातचीत की मांग को लेकर अभियान चला रहे हैं।
रविवार को आंध्र प्रदेश में सिविल सोसाइटी ने फिर अपील की कि उन लोगों से बातचीत शुरू की जाए जो इसके लिए तैयार हैं।
छत्तीसगढ़ में मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों को उठाने वाले नागरिक संगठनों के संयुक्त मंच 'कोऑर्डिनेशन कमेटी फ़ॉर पीस' ने 26 मई को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मांग की कि ‘बसवराजू सहित सभी लोगों के शवों को उनके परिजनों को बिना देरी सौंपा जाए।’
रिपोर्ट्स के मुताबिक़, छत्तीसगढ़ पुलिस ने बसवराजू का शव इसलिए उनके परिवार को नहीं सौंपा क्योंकि उन्हें आशंका थी कि आंध्र प्रदेश के उनके गृह नगर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं।
इसी बीच, संघर्षविराम और शांति वार्ता की मांग लगातार जारी है।
कोलकाता स्थित मानवाधिकार संगठन 'एसोसिएशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ डेमोक्रेटिक राइट्स' के महासचिव रंजीत सूर ने कहा, ‘हम और अन्य मानवाधिकार संगठनों ने दो चरणों की प्रक्रिया की मांग की है पहले संघर्ष विराम और फिर शांति वार्ता।’
इस बीच कड़वेंदी में, रेणुका का परिवार उनकी समाधि के निर्माण को अंतिम रूप देने में जुटा है। ये समाधि डोड्डी कोमुरैया की समाधि से कुछ ही कदम की दूरी पर है।
राजशेखर ने बताया, ‘वारंगल में भारी बारिश हो रही है, इसलिए उद्घाटन में देरी हो रही है।’
अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कड़वेंदी की यह भीषण बारिश कब थमती है। (bbc.com/hindi)