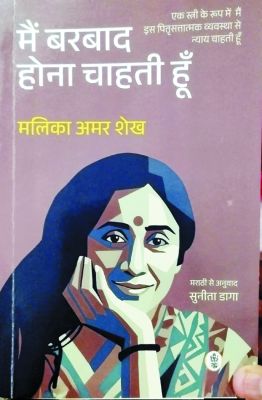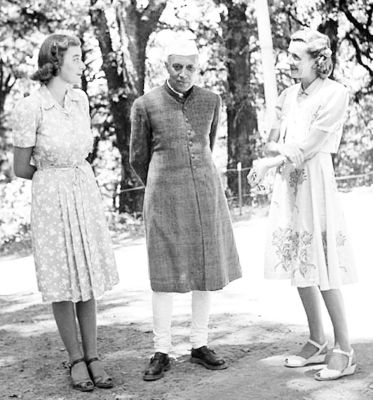विचार / लेख
-आतिफ रब्बानी
बहुत पहले, कऱीब दो दशक पहले, जब लखनऊ से अपने गाँव जाना होता, तो रास्ते में बाराबंकी बस अड्डे पर एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड दिखाई देता था, जिसपर लिखा रहता था- ‘पान खाइए मगर ऐसे नहीं!’ इस इबारत के बैकग्राउन्ड में पान की पीक और इसकी फुहारें-लाल और कत्थई रंगत में पुती रहती थी। यह बिलबोर्ड सालों-साल लगा रहा। आजकल नहीं दिखता है। शायद बाराबंकी के लोग पान खाना ‘सीख’ गए हों। बहरहाल, अजऱ् यह करना है कि इश्तहार में पान खाने की मनाही नहीं थी, बल्कि मनाही थी पीक इधर-उधर थूकने की। पान तो हमारी अज़ीम हिन्दुस्तानी तहज़ीब का हिस्सा है।
पान खाने का एक अपना सलीका हुआ करता है। पान पेश करने की अपनी अदा। पान का मामला नाज़-ओ-अदा का भी है। कोई हसीना पान मुँह में रखे; गिलौरी में महकी हुई बातें करे; दो-शीजग़ी का जलवा हो; बेगमाती लहजे का हल्का-सा छिडक़ाव हो; और फिर आपको पान पेश करे। अहा! क्या कहने! बक़ौल अकबर इलाहाबादी-
लगावट की अदा से उन का कहना पान हाजिऱ है
कय़ामत है सितम है दिल फि़दा है जान हाजिऱ है।
एक ज़माने तक अदब, आदाब और ज़बान-ओ-बयान की एक पूरी तहज़ीब पानदान के आस-पास रही है। बुजुर्गों का अपने से छोटों को पान पेश करना, दोनों हाथ आगे करके पान लेना और तकरीम से सलाम-अलैकुम या आदाब कहना।
घर कोई मेहमान आता तो बड़ी-बूढिय़ाँ अपना पानदान खोलतीं, पान लगातीं और खासदान में पान रखकर इसपर गुंबदनुमा ढक्कन रखकर, मेहमानखाने में पान पहुँचवाती। इज्जत-ओ-एहतराम के साथ, तहजीब-ओ-तकरीम के साथ मेहमानों को पेश किया जाता – कहाँ गए वे दिन!
बात सही है-गंगा-जमुनी ख़ासदान से वकऱ् लगी गिलौरी उठाकर सही लबो-लहजा और अंदाज से आदाब-अर्ज कहने के लिए कई नस्लों का रचाव चाहिए। बक़ौल बशीर बद्र–
सुना के कोई कहानी हमें सुलाती थी
दुआओं जैसी बड़े पान-दान की ख़ुशबू।
आज हमारे कोलीग (और जेएनयू के सीनियर) आलोक भाई ने पान मंगवाया, लेकिन फड़ जमाई गई विपुलजी के चैंबर में (वह भी उनकी गैरमौजूदगी में)। विपुल जी गणित के प्रोफेसर हैं, बहुत फॉर्मूला बताते हैं। अक्सर लोग समझते है कि वह क़ानून के प्रोफ़ेसर हैं। हैं तो वह जन्मना बनारसी ही। बनारसी लोग संगीत, गाली-गुफ़्तारी और पान के बग़ैर अधूरे हैं। लेकिन उनमें ये कोई सिफ़त मौजूद नहीं!
शहनाई के उस्ताद बिस्मिल्लाह खाँ को ही देख लीजिए। दुनिया घूमते थे मगर उनकी रूह को शांति बनारस में ही मिलती थी। गंगा जी के पानी से वज़ू करते, जामा मस्जिद में नमाज पढ़ते, शहनाई और पानदान लेकर बालाजी मंदिर में बैठ जाते थे। कल्ले में गिलौरी दबाई और रियाज शुरू।
यही हाल मौजूदा जमाने में कव्वाल फरीद अयाज़ का है- मुँह में मुलेठी-मिश्रित पान की गिलौरी दबाई और अपने गायन का जादू बिखेरा। क्या कहना! ‘कन्हैया! याद है कुछ भी हमारी।’ अहा! क्या क़व्वाली है! पान बिना मुमकिन नहीं।
वाजिद अली शाह जिन्हें लखनऊ के अवाम प्यार से ‘जाने-आलम’ कहते थे, परीखाना में इंदरसभा सजाते। कृष्ण का रूप इख्तियार करते, रासलीला रचाते और गोपियाँ उन्हें पान पेश करती।
राजपूतों के सेनापति हथेली पर बीड़ा यानी पान रखकर पीछे खड़े कमांडरों और सैनिकों से पूछते- ‘है कोई राजपुताना की माटी का जाँबाज़ जो उतरे मैदान में?’ जो कमांडर आगे बढक़र हथेली से बीड़ा उठा लेता वह दरअसल मार्का अपने सर ले लेता। जंग में फ़तह के लिए बेकरार हो उठता। जान लगा देता। इसी रस्म से जिम्मेदारी उठाने के लिए ‘बीड़ा उठाने’ का मुहावरा चल निकला। आलोक सर ने आज बीड़ा तो उठवाया लेकिन अभीतक अपने इरादे जाहिर नहीं किए!
पानदान कभी हमारी तहजीब का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ तक की घर में कोई नई बहू बियाह कर आती तो लाज़मी तौर पर जहेज में पानदान भी लाती थी। लेकिन अब आज के ‘मॉडर्न’ दौर में वैसे कितने लोग रह गए होंगे जो अब भी पानदान रखते होंगे; जिन्हें कत्था पकाना और छानना आता होगा; पान पलटने का सलीक़ा आता होगा; चूने की तरकीब जानते होंगे; सरौते से डली और मेवा काटते होंगे?
‘सरौता कहाँ भूल आए प्यारे नंदोईया’ जैसे गाने ना-पैद हुए।
अब न ढोलकियों में वो थाप रही, और ना सरौते में वो काट रही! पानदान रुख़स्त हुआ तो उसके गिर्द घूमती हुई तहज़ीब भी साथ ही रुखस्त हो गई। वज़्अ-दारी, लहजा और जबान भी रुखस्त हो गए।
अब न रहे वो पीने वाले,
अब न रही वो मधुशाला।
हाँ, अब यहाँ एक बात कहनी जरूरी हो गई है- तंबाकू, जर्दा, गुटखा और पानमसाला-जैसे ज़हर को लोग पान समझ बैठे हैं। ये पान नहीं है। रही यहाँ-वहाँ पड़ी पीकों की पिचकारियाँ, तो इसमें पान का हरगिज कोई कसूर नहीं है। सारा क़सूर हमारी तमीज़, तर्बियत, तहज़ीब और संस्कार का है। पान जरूर खाइए, मगर ऐसे नहीं।