ताजा खबर

पूरी दुनिया में गांवों से शहरों की ओर लोगों का जाना एक नजर में इसलिए नहीं दिखता है कि गांव बहुत छोटे-छोटे हैं, बिखरे हुए हैं, वहां से लोगों का जाना वहां के बाकी लोगों को तो दिखता है, लेकिन बाहर के लोगों को नहीं दिखता। दूसरी तरफ शहरों में यह बात कुछ अधिक आसानी से दिखती है क्योंकि वहां गांवों से आए हुए लोगों की बसाहट शहर के किनारे-किनारे बढ़ती जाती है, शहर की बढ़ती जरूरतों के लिए मजदूरों की मौजूदगी भी बढ़ती ही रहती है। इस एक तस्वीर के दो अलग-अलग पहलू हैं। और इन दोनों को मिलाकर देखें, तो ऐसा लगता है कि बढ़ता शहरीकरण दुतरफा असर डाल रहा है, गांवों को नजरों से परे की हद तक प्रभावित कर रहा है, और वहां से शहर आने वाले लोगों की जिंदगी को भी सामान्य से अधिक हद तक।
गांवों से शहरों की तरफ लोगों के जाने की सबसे बड़ी वजह रोजगार की तलाश में होती है। गांवों तक मनरेगा जैसी योजनाएं पहुंची थीं, जिन्होंने लोगों को गांवों में बने रहने की एक छोटी सी संभावना दी थी, सहारा दिया था, लेकिन अब सुनते हैं कि इस योजना के जी राम जी हो जाने के बाद ऐसी संभावनाओं को जय राम जी हो जाने की आशंका बढ़ गई है। केन्द्र सरकार ने योजना में जिस तरह के फेरबदल किए हैं, उनसे कई लोगों को लगता है कि राज्य अपने ऊपर बढ़े हुए ऐसे बोझ को अधिक नहीं ढो पाएंगे। खैर, इस योजना पर चर्चा आज का मकसद नहीं है, आज का मकसद गांवों से शहर आने की मजबूरी है।
यह भी समझने की जरूरत है कि जिन लोगों ने गांव को भोगा नहीं है, उन्होंने गांव को भुगता भी नहीं है। गांव जाति व्यवस्था के, संयुक्त परिवार व्यवस्था के, संपन्नता और विपन्नता के बड़े उदाहरण रहते हैं। गांवों को लेकर जितनी रोमांटिक तस्वीर बनती है, हकीकत उतनी ही क्रूर रहती है। कुछ लोगों को गांव प्रेमचंद की कहानियों सरीखे लग सकते हैं, और कुछ अधिक लोगों को गांव श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी के बैद जी के गांव या कस्बे सरीखे मिल सकते हैं। जाति व्यवस्था से, और दूसरे शोषण-अत्याचार से थककर भी कुछ लोग शहरों की ओर चले जाते हैं, गांव कभी न लौटने के लिए।
छत्तीसगढ़ जैसे राज्य ने एक वक्त सूखे महीनों में लाखों या दसियों लाख लोगों का प्रदेश से बाहर जाना देखा है। हो सकता है कि सरकार ने कभी भी इन आंकड़ों को पूरी सच्चाई के साथ उनकी असली हद तक दर्ज न किया हो क्योंकि सरकारी अमले के हाथों शोषण से बचने के लिए अधिकतर लोग सरकार को खबर किए बिना ही बाहर जाते थे, और आज भी उसी तरह जाते हैं। लेकिन इनके मुकाबले थोड़े से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि मजबूरी के विस्थापन वाले न हों, और बेहतर रहन-सहन, अधिक शहरी सुविधाओं, पढ़ाई-लिखाई या इलाज के लिए बाहर जाते हों। जो भी हो, आज पूरी दुनिया में गांवों की आबादी घटती चल रही है, और शहरों के बारे में बेरहम जुबान में कहा जाता है कि उन पर बोझ बढ़ते चल रहा है।
गांवों से लोगों के निकल चले जाने का हाल भारत के ही कुछ पहाड़ी राज्यों से लेकर पश्चिम के कई देशों तक ऐसा है कि अच्छे-खासे बसे हुए गांव अब घोस्ट टाऊन कहलाते हैं, यानी भुतहा गांव या कस्बा। हिन्दुस्तान में भी हिमाचल तरफ कई ऐसे गांवों की कहानियां आती हैं जिनमें गिने-चुने लोग रह गए हैं, बाकी सारे चले गए हैं। पश्चिम के कुछ देशों में ऐसे गांवों में आकर बसने के लिए सरकार कुछ अनुदान भी दे रही है। जब गांवों के उजाड़ होने की नौबत इतनी भयानक है, तो यह भी समझने की जरूरत है कि क्या इंसानों के अलावा भी गांवों को कुछ और छोडक़र जाते हैं?
गांवों की अपनी एक अलग संस्कृति रहते आई है, वहां के रीति-रिवाज, त्यौहार, सामाजिक परंपराएं, लोक कथाएं, लोकगीत और संगीत, लोककला जैसी बहुत सी जिंदगी की महीन ऐसी बातें हैं जो कि सरकारी जनगणना के आंकड़ों में कहीं नहीं आतीं, लेकिन जब गांव उजड़ते हैं, तो इनमें से तमाम बातें भी उजडऩे लगती हैं। अब कल्पना करें गांव की एक ऐसी संगीत टोली का, जिसके एक-दो वादक या गायक गांव छोडक़र चले गए, तो बाकी का क्या होगा? ऐसे विलेज-बैंड के लोग पूरी तरह से गाने-बजाने पर जिंदा नहीं रहते, वे दूसरे काम भी करते हैं। अब अगर ऐसे दूसरे काम छिन गए, उन्हें काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा, तो कुछ लोगों के बाहर जाने से बैंड के बाकी लोग भी बेकार हो गए, और हो सकता है कि उस गांव की लोक संगीत की एक परंपरा ही टूट जाए।
यह भी सोचें कि अगर गांव के किसी भित्ति चित्रकार को काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा, तो गांव में उसके साथ काम कर-करके जो सहायक इस शैली को सीख रहे थे, वही खत्म हो गई, तो क्या होगा? उसके दुबारा जिंदा होने की संभावना कम ही रहती है। लोग कम होते जाते हैं, तो सभी समारोह भी कम होने लगते हैं, और परंपराएं कमजोर पडऩे लगती हैं।
इसलिए यह समझने की जरूरत है कि गांव को महज आबादी छोडक़र नहीं जाती, उस गांव की संस्कृति, परंपराएं, रीति-रिवाज, और हर किस्म की लोककला, लोक साहित्य, सभी कुछ छोडक़र चले जाने का एक खतरा रहता है। दूसरी तरफ जब यही आबादी देश भर के अलग-अलग शहरों में बिखर जाती है, तो हां पर एक नई अर्थव्यवस्था में जिंदा रहने की चुनौती इतनी बड़ी रहती है, लोग इतने दूर-दूर छिटक गए रहते हैं कि वहां पर वे अपनी ग्रामीण परंपराओं को जारी नहीं रख पाते, अगली पीढ़ी तो उसके बिना ही बड़ी होती चलती हैं, और परंपराओं से उसका रिश्ता कायम ही नहीं हो पाता।
अब हम इस सिक्के के दूसरे पहलू को देखें, तो गांवों से शहर पहुंचने वाले लोग एक अंधाधुंध गर्मी, और प्रदूषण के बीच भी पहुंच जाते हैं। यहां लिखने का मतलब सांस्कृतिक प्रदूषण नहीं है, सांस लेने वाली हवा का प्रदूषण है। गर्मी वह गर्मी है जो कि शहरी संपन्नता के एयरकंडीशनरों से निकलकर फैलती है, और खुले में जीने को बेबस मजदूरों को हासिल हवा को और गर्म करती है। गरीबों के आने-जाने की कोई भी गाडिय़ां एसी तो रहती नहीं हैं, इसलिए फुटपाथों पर जीते हुए, लालबत्तियों के इर्द-गिर्द ट्रैफिक के धुएं के बीच काम करते हुए, कहीं निर्माण स्थल पर निर्माण-प्रदूषण को सीधे झेलते हुए, कहीं छोटे-बड़े कारखानों, और भट्टियों के आसपास रहते हुए गांव से आए हुए गरीब मजदूर, पहले से बसे हुए शहरी मजदूरों के साथ-साथ शहरी धूल, धुएं, धूप, और बाकी प्रदूषण के गुबार को झेलते हैं।
एक तरफ उनका छोड़ा हुआ गांव संस्कृति को खोने के खतरे में पड़ चुका रहता है, दूसरी तरफ शहरों में पहुंचे हुए इन ग्रामीणों की सेहत असहनीय शहरी हालात का शिकार रहती है। ये ग्रामीण अपने गांवों से दूर कुछ अलग किस्म से झुलसते हैं, दूसरी तरफ गांव की संस्कृति एक अलग किस्म से झुलसती है। इन दोनों में अगर आपको कोई रिश्ता दिखता है, तो आप देख सकते हैं, वरना ये एक सिक्के के दो अलग-अलग पहलू हैं जो कि एक साथ नहीं दिख पाते, लेकिन इन दोनों को मिलाकर ही सिक्का पूरा होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह कि गांवों से शहरों की तरफ के विस्थापन से ही आज की यह दुनिया पूरी होती है। अपना कहे जाने वाले गांव को छोडक़र निकलना, और पराया समझे जाने वाले शहर में बसना, बहुत से लोगों के लिए यह आगे बढऩे का एक सिलसिला होता है। जिंदगी की रोज की लड़ाई में जिंदा रह पाना अधिकतर लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण और जरूरी होता है कि गांव से जुड़ी हुई संस्कृति और वैसी दूसरी महीन बातों को ढोने के लिए उनके कंधों पर न जगह बचती है, न रीढ़ की हड्डी में उतनी ताकत।
गांव और शहर के बीच के इंसान को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं, अलग-अलग कवि, लेखक, और पत्रकार की नजर से देखने पर यह एक ही इंसान कई अलग-अलग इंसान की तरह दिखते हैं। देखते हैं कि आपको इनमें से कौन सा इंसान दिखता है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)







.jpg)


.jpg)



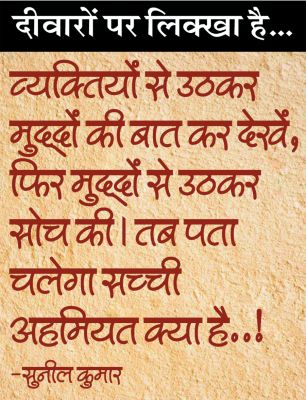

.jpeg)
