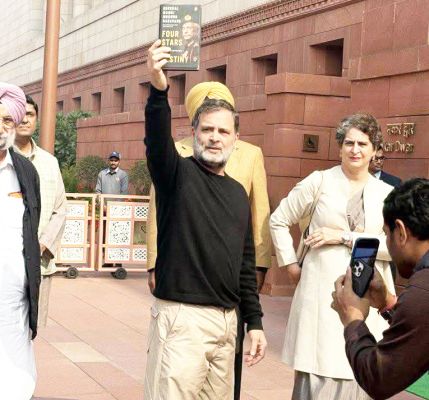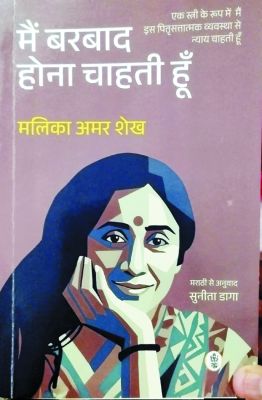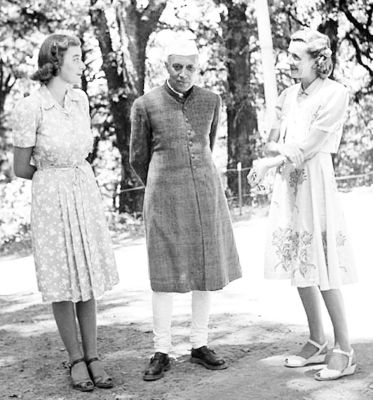विचार / लेख
इन दिनों राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और त्रिभाषा फॉर्मूले बनाम द्विभाषा नीति पर राष्ट्रव्यापी विवाद छिड़ा है। यह विवाद तब शुरु हुआ, जब केंद्र ने तमिलनाडु को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि 2,152 करोड़ रुपये रोक ली। इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक राज्य को समग्र शिक्षा अभियान की कोई राशि जारी नहीं की है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए इस फंड की जरूरत है और इसे तुरंत रिलीज करने की मांग की।
इसके बाद से इस विवाद पर उत्तर और दक्षिण भारत के कई राजनेताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के विचार सामने आए हैं। इनमें तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा मंत्री पलानीवेल त्याग राजन, वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे, स्वराज इंडिया के संस्थापक और भारत जोड़ो आंदोलन के राष्ट्रीय समन्वयक योगेंद्र यादव और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अपूर्वानंद शामिल हैं। इनकी राय को ‘हरकारा’ के विशेष पेज पर जगह देकर हमने यह समझने की कोशिश की है कि यह विवाद क्या है और इसका क्या संभावित हल हो सकता है।
इस बहस को आगे बढ़ाते हुए स्टालिन ने मंगलवार 4 मार्च को एक्स पर लिखा, ‘तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों ने उत्तरी राज्यों पर अपनी भाषाएँ सीखने का कभी दबाव नहीं डाला। दक्षिण भारतीयों को हिंदी सिखाने के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किए एक सदी बीत चुकी है। इन सभी वर्षों में उत्तर भारत में कितनी उत्तर भारत तमिल प्रचार सभाएँ स्थापित की गई हैं? सच तो यह है कि हमने कभी यह मांग नहीं की कि उत्तर भारतीयों को तमिल या कोई अन्य दक्षिण भारतीय भाषा सीखनी चाहिए, ताकि उन्हें 'संरक्षित' किया जा सके। हम बस इतना ही चाहते हैं कि हम पर प्तस्ह्लशश्च॥द्बठ्ठस्रद्बढ्ढद्वश्चशह्यद्बह्लद्बशठ्ठ न हो। अगर भाजपा शासित राज्य 3 या 30 भाषाएँ सिखाना चाहते हैं तो उन्हें करने दें! तमिलनाडु को अकेला छोड़ दें!’
इसके पहले मुख्यमंत्री स्टालिन ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान की आलोचना की थी, जिसमें प्रधान ने यह कहा था कि तमिलनाडु को भारतीय संविधान की शर्तों को मानना होगा और त्रिभाषा नीति ही कानून का शासन है। जब तक तमिलनाडु एनईपी और त्रिभाषा फार्मूले को स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक प्रदेश को समग्र शिक्षा अभियान के तहत फंड नहीं उपलब्ध कराया जाएगा।
द हिंदू के अनुसार, स्टालिन ने यह भी कहा है कि हिंदी सिर्फ मुखौटा है और केंद्र सरकार की असली मंशा संस्कृत थोपने की है। उन्होंने कहा कि हिंदी के कारण उत्तर भारत में अवधी, बृज जैसी कई बोलियां खत्म हो गईं। राजस्थान का उदाहरण देते हुए स्टालिन ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार वहां उर्दू हटाकर संस्कृत थोप रही है। अन्य राज्यों में भी ऐसा होगा इसलिए तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है।
इसी के आलोक में ‘द वायर’ के लिए करण थापर से बात करते हुए तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा मंत्री पलानीवेल त्याग राजन ने त्रिभाषा फॉर्मूला पर अपने विचार रखते हुए कहा कि उनका मानना है कि वित्तपोषित तमिलनाडु राज्य बोर्ड के तहत स्कूली शिक्षा प्रणाली और तमिलनाडु सरकार की ओर से शिक्षा की निर्धारित रूपरेखा बहुत स्पष्ट है। इसमें केवल दो भाषाओं की आवश्यकता है। वह कहते हैं कि राज्य वित्तपोषित बोर्ड के स्कूलों में दो से अधिक भाषाओं को पढ़ाना अनिवार्य नहीं करेंगे। हम महसूस कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ें नहीं सुनी जा रही हैं। वे हमें यह कहकर जबरन वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको हिंदी सीखनी होगी, जो हमारे प्रदर्शन के विपरीत है।
उन्होंने कहा, ‘हम आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में ले जाने के विरोध में थे। हमने हमेशा से ही महसूस किया है कि शिक्षा को राज्य का विषय होना चाहिए। अच्छी खबर यह है कि हमने इस देश के लगभग किसी भी अन्य राज्य की तुलना में उल्लेखनीय परिणाम दिखाए हैं। हम नहीं मानते कि तमिलनाडु के बाहर किसी को भी हमें यह बताना चाहिए कि राज्य की स्कूल शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए। पहली समस्या, पहला मुद्दा यह एक समवर्ती विषय है। प्रारंभिक शिक्षा किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक हमेशा से विशेष रूप से राज्य का विषय था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और पूरे देश में डिग्री के मान्य होने की आवश्यकता के कारण हम उच्चतर शिक्षा के आधे स्पेक्ट्रम को एक तरह से समवर्ती सूची के रूप में देख सकते हैं।
त्रिभाषा फॉर्मूला में हिंदी नहीं थोपने की बात पर वह कहते हैं कि मैंने दस्तावेज पढ़ा है। यह कई जगह हिंदी और संस्कृत की बात करता है। हम विधायक हैं। हम चुने जाते हैं। हम सरकार बनाते हैं। हमारी एक सरकारी नीति है। हमारी नीति दो भाषा नीति है। हम तीन भाषा नीति नहीं चाहते हैं। यह जातीय, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से एक परिष्कृत दृष्टिकोण है, जिसने शानदार परिणाम दिए हैं।
उत्तर भारतीय राज्यों में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू होने पर वह कहते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश में कितने बच्चे तीन भाषाएं जानते हैं? इन प्रदेशों में कितने बच्चे दो भाषाएं जानते हैं? पिछले 75 वर्षों में हमारे देश में इसके क्या परिणाम रहे हैं? हमारे कितने प्रतिशत बच्चे दो भाषाओं में बहुत अच्छे हैं? आपका मतलब बच्चे सीखने में बहुत अच्छे होते हैं से है, यह दिखाने के लिए परिणाम कहां हैं! मुझे एक जगह बताएं, जहां इस देश में तीन भाषा फॉर्मूला ने तमिलनाडु राज्य से बेहतर परिणाम दिए हों।
वह यह भी कहते हैं, "‘ऐसा नहीं है कि त्रिभाषा फॉर्मूला हमें पहले स्वीकार था और अब नहीं है। आप कहते हैं कि त्रिभाषा फॉर्मूला शिक्षा नीति की पहली पंक्ति है। मैं कहता हूँ कि 75 वर्षों से या यों कहें कि 1952 से तमिलनाडु या मद्रास राज्य की सरकार के समय से हमारे पास कभी त्रिभाषा फॉर्मूला नहीं था।’
मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार जहां त्रिभाषा फॉर्मूला लागू है, वहां के बच्चे एक भाषा में भी पारंगत नहीं हैं। बिना किसी सफल कार्यान्वयन के कहीं भी, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि हमें दो भाषाओं की मूल मान्यता को छोड़ देना चाहिए। हमारे पास 70 साल का डेटा है, परिणाम हैं।
इस विवाद पर उत्तर भारत के कुछ लेखकों, समीक्षकों और शिक्षाविदों की टिप्पणियां भी आई है। उनमें से एक वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे का कहना है कि वह उन भारतीयों की हिंदी आलोचनाओं से दुखी और क्रोधित हैं, जो अंग्रेजी बोलते हैं और ‘हिंदी थोपे जाने’ के खिलाफ चिल्लाते हैं। इनमें हिंदीपट्टी के कई शिक्षित भारतीय शामिल हैं। जब बात अपने बच्चों की आती है तो माता-पिता - जिनमें भाजपा नेतृत्व और हिंदी के सबसे मुखर समर्थक भी शामिल हैं - अपेक्षाकृत महंगे निजी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के पक्षधर होंते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला देश बनने की राह पर है, जहां युवा तेजी से सोशल मीडिया पर सांस्कृतिक अज्ञानियों की भीड़ में तब्दील होते जा रहे हैं।
पांडे के अनुसार, जो लोग गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों से हैं, वे हिंदी थोपे जाने को कोसते हुए ईमानदारी से आत्मचिंतन नहीं करेंगे कि वे अपनी मूल भाषा बांग्ला, तमिल, कन्नड़ या उडिय़ा में अपनी पुस्तकें क्यों नहीं लिख पाए। हिंदी और उर्दू के साहित्यिक इतिहासकारों की बात करें तो वे भी हिंदी और उर्दू के लिए गुस्से से भरी प्रतिस्पर्धी ऐतिहासिक कहानियाँ लिखने में ही उलझे रह गए हैं। भारतीय साहित्य का एक शांत, समग्र, व्यापक इतिहास जो हिंदी और उर्दू दोनों को लोगों की भाषाओं के रूप में फैलाता है, जिसमें सिर्फ लिपि में अंतर है, अभी तक नहीं लिखा गया है। पांडे लिखती हैं, 20वीं सदी से पहले भारत एक बहुभाषी राष्ट्र था। प्रत्येक क्षेत्र की एक भाषा थी। प्रत्येक भाषा की मौखिक साहित्य और क्षेत्रीय बोलियों की अपनी परंपरा थी।
‘भाषा या भाखा’ हमेशा से उत्तरी मैदानों में बोली जाने वाली बोलियों के समावेशी मिश्रण के लिए शब्द रहा है : ब्रज, अवधी, कौरवी, मैथिली, भोजपुरी आदि। 13वीं शताब्दी के आसपास, हिंदी का यह प्रोटोटाइप धीरे-धीरे दक्षिण की ओर बढऩे लगा था, जिसका श्रेय रामानंद की ओर से उत्तर में शुरू किए गए दो-तरफा आंदोलन को जाता है। किसी ने तब इसे उत्तर या दक्षिण में ‘थोपने’ के रूप में नहीं देखा।
जिस हिंदी को आज सरकार राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना चाहती है, वह संस्कृत से जुड़ी हुई है, जिसमें जातिवाद का सारा बोझ बरकरार है। और इसकी अत्यधिक सहयोगी शब्दावली का उपयोग बोलियों, इस्लामी और यूरोपीय भाषाओं से सदियों से आत्मसात किए गए हजारों शब्दों को ‘शुद्ध’ करने के लिए किया जा रहा है, ताकि ‘शुद्ध, स्वच्छ हिंदी’ का अंतिम खाका तैयार किया जा सके। यह विडंबना है कि जब से भाजपा ने इसे फिर से जगाया है, तब से भाषा के मुद्दे पर दोनों पक्षों में तलवारें खिंच रही हैं।
वहीं स्वराज इंडिया के संस्थापक और भारत जोड़ो आंदोलन के राष्ट्रीय समन्वयक योगेंद्र यादव का मानना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि त्रिभाषा फार्मूले (टीएलएफ) को लेकर डीएमके सरकार के पास नाराज़ होने और संदेह के ठोस कारण हैं। मोदी सरकार ने बार-बार संघवाद की भावना का उल्लंघन किया है। तमिलनाडु के राज्यपाल बेशर्मी से भाजपा की ओर से काम कर रहे हैं। मोदी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में राज्य सरकारों की शक्तियों का बार-बार अतिक्रमण किया है। कुलपतियों की नियुक्ति की नीति इसका ताजा उदाहरण है। यह भी सही है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को शिक्षा नीति अपनाने के लिए मजबूर करने के लिए केंद्रीय धन का इस्तेमाल छड़ी के रूप में नहीं कर सकती, वह भी भाषा के चयन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर।
अब तो टीएलएफ के तहत बच्चों को राज्य द्वारा चुनी गई कोई भी तीन भाषाएँ सिखाई जानी चाहिए, बशर्ते तीन में से दो ‘मूल भारतीय’ भाषाएँ हों। इसलिए, यदि तमिलनाडु चाहे, तो वह तमिल के साथ-साथ मलयालम या तेलुगु या कन्नड़ या शास्त्रीय तमिल और अंग्रेजी भी पढ़ा सकता है।
त्रिभाषा फॉर्मूले पर मूल सहमति यह थी कि हिंदी भाषी राज्य एक और आधुनिक भारतीय भाषा, अधिमानत: एक दक्षिण भारतीय भाषा पढ़ाएं। शुरुआत में, यूपी में तमिल, हरियाणा में तेलुगू आदि पढ़ाने की कुछ योजनाएँ थीं, लेकिन जल्द ही हिंदी राज्यों ने शॉर्टकट ढूंढ़ लिया। संस्कृत या बल्कि भाषा की ‘एक प्राथमिक और यांत्रिक रटना’ सीखने को ‘तीसरी भाषा’ के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार किसी अन्य लिपि या भाषा को सीखने की आवश्यकता को दरकिनार कर दिया गया। इसलिए प्रभावी रूप से, टीएलएफ एक असमान सौदा बन गया। इस धोखे को उजागर करने का समय आ गया है। इस तरह के कदम से यह सरल तथ्य उजागर हो सकता है कि यह तमिलनाडु नहीं, बल्कि वे हिंदी राज्य हैं, जिन्होंने टीएलएफ को नुकसान पहुंचाया है।
(‘हरकारा'’ यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूजलेटर से यह लेख साभार।)