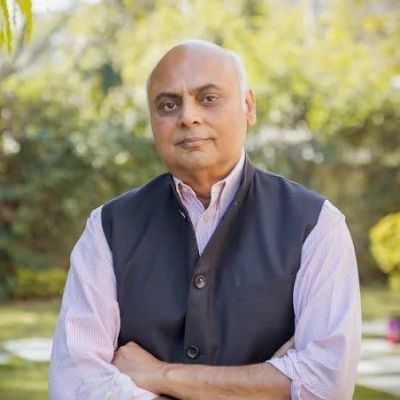विचार / लेख
पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्लभ प्रजाति में शामिल रेड पांडा के संरक्षण की दिशा में अहम कदम उठाया है. दार्जिलिंग के सिंगालीला नेशनल पार्क में नौ रेड पांडा खुले में छोड़े गए हैं ताकि प्रजनन के जरिए उनकी आबादी बढ़ाई जा सके.
 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट -
डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट -
भारत में रेड पांडा को बचाने की एक बड़ी कोशिश जारी है. इसके लिए कई स्तर पर प्रयास हो रहे हैं. रेड पांडा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजाति के तौर पर शामिल है. भारत में यह जानवर दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र के अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है. दार्जिलिंग के डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर यानी डीएफओ (वाइल्डलाइफ डिवीजन) विश्वनाथ प्रताप बताया कि सेंचल वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी और सिंगालीला नेशनल पार्क में फिलहाल करीब 40 रेड पांडा हैं.
दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में रेड पांडा को देखने के लिए पर्यटकों और पशु प्रेमियों की भारी भीड़ जुटती है. आम तौर पर शर्मीला माना जाने वाला यह जानवर ऊंचे पेड़ों या पार्क में बनी कंदराओं में रहता है. इस चिड़ियाघर को भी वर्ष 2022 में देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का तमगा मिल चुका है.
गुजरात के वनतारा जू पर फिर हुआ विवाद
वहीं इस दौरान सिक्किम स्थित हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में भी सात वर्षों के बाद इस साल रेड पांडा के दो शावकों का जन्म हुआ है. इसे इस जीव के संरक्षण की दिशा में अहम प्रगति माना जा रहा है. अब दार्जिलिंग के सिंगालीला नेशनल पार्क में नौ रेड पांडा खुले में छोड़े गए हैं ताकि प्रजनन के जरिए उनकी आबादी बढ़ाई जा सके. वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी विश्वनाथ प्रताप डीडब्ल्यू को बताते हैं, "जिन रेड पांडा को सिंगालीला नेशनल पार्क में खुले में छोड़ा गया था उन्होंने नए माहौल से तालमेल बिठा लिया है."
साझा संरक्षण अभियान
रेड पांडा के संरक्षण के लिए राज्य वन विभाग पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के साथ संयुक्त रूप से रेड पांडा कैप्टिव ब्रीडिंग एंड री-इंट्रोडक्शन कार्यक्रम चला रहा है. इस कार्यक्रम का मकसद चिड़ियाखाना में पैदा होने वाले रेड पांडा के शावकों को जरूरी ट्रेनिंग के बाद खुले में छोड़ना है ताकि उनकी आबादी बढ़ाई जा सके. दार्जिलिंग जिले के सिंगालीला और नेवड़ा वैली नेशनल पार्क को इस जीव के सुरक्षित, संरक्षित आवासीय क्षेत्र के तौर पर चुना गया है. वन विभाग ने इलाके में निगरानी भी तेज की है ताकि उनको शिकारियों के हाथों से बचाया जा सके.
वन विभाग के एक अधिकारी डीडब्ल्यू को बताते हैं, "पार्क के आस-पास बसे गांवों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि इस लुप्तप्राय प्रजाति के जीव के संरक्षण में मदद मिले और इनकी आबादी बढ़ाई जा सके."
वो बताते हैं, "इन दोनों नेशनल पार्क में रेड पांडा की सही तादाद का पता लगाने के लिए उनकी गिनती का काम भी चल रहा है. हालांकि इस जीव के ऊंचे पेड़ों पर रहने और कंदराओं में छिपने की वजह से यह काम कुछ मुश्किल है. लेकिन इसमें ड्रोन और आधुनिक तकनीक की मदद ली जा रही है."
पद्मजा नायडू पार्क के निदेशक अरुण कुमार मुखर्जी डीडब्ल्यू को बताते हैं, "हमारे रेड पांडा संरक्षण कार्यक्रम को वैश्विक सराहना मिली है. बीते दो साल के दौरान तीन मादा रेड पांडा ने नेशनल पार्क में पांच शावकों को जन्म दिया है. अब राज्य सरकार के सहयोग से दोनों नेशनल पार्क में संरक्षण के लिहाज से कई बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं."
उन्होंने बताया कि संरक्षण के इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदायों को शामिल करने का भी प्रयास किया जा रहा है.
आनुवंशिक बायोबैंक की स्थापना
पद्मजा नायडू पार्क इस जीव के संरक्षण के लिए टोपकेदारा संरक्षण केंद्र का संचालन करता है. पार्क के निदेशक अरुण कुमार मुखर्जी बताते हैं, "हमने बीते दो साल के दौरान दस रेड पांडा खुले जंगल में छोड़े हैं. हमारी योजना अगले पांच साल में कम से कम 20 रेड पांडा को जंगल में छोड़ने की है."
पार्क ने इस साल जून में रेड पांडा, स्नो लेपर्ड और हिमालयन तहर जैसे लुप्तप्राय जानवरों के डीएनए और आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करने के लिए एक आनुवंशिक बायोबैंक की स्थापना की थी. यह ऐसा करने वाला देश का पहला केंद्र है.
अलग हैं रेड पांडा
बीते कई साल से रेड पांडा के संरक्षण और उनकी आदतों पर शोध करने वाली मौमिता चक्रवर्ती डीडब्ल्यू को बताती हैं, "यह जीव कई मायनों में दूसरे जीवों से अलग है. रहने की जगह का सिकुड़ना रेड पांडा की आबादी घटने की अहम वजहों में से एक है."
मौमिता के मुताबिक, रेड पांडा भोजन के लिए मुख्य रूप से बांस के पत्तों और कोमल कोंपलों पर निर्भर रहते हैं और उनकी जैविक संरचना इसी के अनुकूल है. रेड पांडा की जीवनशैली और सर्दी के सीजन में मेटाबॉलिज्म कम करने की क्षमता उनको हिमालय की कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रखती है.
पार्क के निदेशक अरुण कुमार बताते हैं, "दार्जिलिंग जैसे पर्वतीय इलाके में होने की वजह से हमारे पास इस पार्क के विस्तार की जगह नहीं है. हम ऊपरी इलाकों को संरक्षण के लिए विकसित कर रहे हैं."
वन्यजीव प्रेमियों ने सरकार की इस पहल पर खुशी जताई है. सिलीगुड़ी में एक वन्यजीव संगठन के संयोजक शिशिर कुमार भादुड़ी डीडब्ल्यू से कहते हैं, "यह सराहनीय पहल है. रेड पांडा दार्जिलिंग समेत पूरे बंगाल की शान है. इस के संरक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए"
एक वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्ता सुलग्ना चटर्जी कहती हैं, "रेड पांडा के संरक्षण पर और ज्यादा ध्यान देना जरूरी है. इस लुप्तप्राय जीव के लिए दार्जिलिंग का मौसम और माहौल एकदम मुफीद है. संरक्षण के साझा प्रयासों से आबादी बढ़ा कर ही इसे विलुप्त होने से बचाया जा सकता है."
ये है सबसे दुर्लभ व्हेलों में से एक, आबादी केवल 384
नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल, सबसे दुर्लभ व्हेलों में से एक है. इनकी अनुमानित आबादी है, मात्र 384. अच्छी खबर ये है कि इनके संरक्षण की कोशिशें रंग ला रही हैं.
इस बरस कितनी आबादी बढ़ी?
यह एक बेहद दुर्लभ व्हेल प्रजाति है. साल 2024 तक दुनिया में नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल प्रजाति के केवल 376 सदस्य ही मौजूद थे. इस साल इनकी जनसंख्या में आठ नए सदस्यों की आमद हुई है और अब इनकी आबादी 384 हो गई है. 'नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल कंसोर्टियम' की एक नई रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है.
इसे अपना नाम कैसे मिला?
वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फाउंडेशन (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) के मुताबिक, इस प्रजाति के नाम में जो "राइट" शब्द है, उसका अतीत शिकार से जुड़ा है. व्हेलों का शिकार करने वाले शुरुआती लोग उन्हें शिकार के लिए "सही और मुफीद" पसंद मानते थे. इस तरह प्रजाति के नाम में ही "राइट" जुड़ गया.
नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल को कैसे पहचानें?
'नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल' प्रजाति के वयस्क की लंबाई 45 से 55 फीट और वजन लगभग 70 टन तक हो सकता है. शरीर गहरे सलेटी रंग का और सिर के ऊपर की त्वचा पर सफेद रंग का पैच (कैलेस) होता है. ये सफेद रंग इनकी सबसे खास पहचान है. डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के मुताबिक, विशाल व्हेलों की सबसे संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक हैं नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल.
तेजी से घटती गई आबादी
पिछले दशक में 'नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल' की जनसंख्या बहुत चिंताजनक तरीके से कम हुई. केवल साल 2010 से 2020 के बीच ही इनकी आबादी में करीब 25 प्रतिशत की कमी आई. समुद्र में जहाजों से टकराना या मछली पकड़ने वाले उपकरणों में फंस जाना इन व्हेलों के लिए बड़ा खतरा है. मसलन, जाल अगर मुंह के पास लिपटा हो तो ये खाना नहीं खा सकेंगे या खाना खाने में दिक्कत होगी. या, सतह पर सांस नहीं ले पाएंगे.
कब शुरू हुआ संरक्षण?
मांस और तेल जैसी चीजों के लिए व्यावसायिक स्तर पर व्हेलों के शिकार (व्हेलिंग) से इस प्रजाति को बहुत नुकसान पहुंचा, जिससे वो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए. डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के मुताबिक, 1930 के दशक में इन व्हेलों को व्यावसायिक व्हेलिंग से सुरक्षा मिली. मगर दशकों तक इनकी स्थिति में सुधार नहीं आया. अब ये ज्यादातर उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक तट के आसपास पाए जाते हैं.
आबादी बढ़ रही है, मगर धीरे-धीरे
अब इनके संरक्षण की नई कोशिशें थोड़ा असर दिखा रही हैं. इन विशालकाय जीवों की निगरानी करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि इन व्हेलों की जनसंख्या में हो रहा इजाफा उत्साह बढ़ाने वाला है. साल 2020 से अब तक इनकी जनसंख्या में सात प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हुई है. खासतौर पर पिछले चार साल से इनकी आबादी में बढ़ोतरी का ट्रेंड नजर आ रहा है.
समुद्र में बढ़ता ट्रैफिक भी एक परेशानी है
वैज्ञानिकों के मुताबिक, व्हेलों में प्रजनन पहले से काफी कम हुआ है. इसकी कई वजहें हो सकती हैं. मसलन, समुद्र में जहाजों की आवाजाही बढ़ गई है. व्यस्त रास्तों पर आने-जाने में व्हेलों को दिक्कत होती है. इसके अलावा उनके आहार के स्रोतों की उपलब्धता भी घट रही है. पूरी खुराक ना मिलने या घायल होने की हालत में भी व्हेलों के प्रजनन की संभावना कम हो जाती है.
समुद्र में बढ़ता शोर भी नुकसानदेह
समुद्र में जहाजों की आवाजाही से पानी के भीतर शोर पैदा होता है. 2012 में हुई एक स्टडी से संकेत मिला कि इसके कारण व्हेलों की संवाद करने की क्षमता में खलल पड़ रहा है. पता चला कि इस शोर के कारण एक-दूसरे को सुनने में व्हेलों को बहुत दिक्कत हो रही है. यह प्रजनन के लिए साथी खोजने, सुरक्षित आवाजाही करने, खाने की तलाश, शिकारियों से बचाव और बच्चों की देखभाल की उनकी क्षमता को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है.
... और क्लाइमेट चेंज तो खतरा है ही
दुनिया गर्म हो रही है, समुद्र और तेजी से गर्म हो रहा है. जलवायु परिवर्तन ने भी इन व्हेलों की प्रजनन दर को प्रभावित किया है. यह व्हेलों के आहार स्रोत को प्रभावित कर रहा है. क्लाइमेट चेंज ना केवल समुद्री पानी के तापमान को बदल रहा है, बल्कि हवाओं और समुद्री तरंगों पर भी असर डाल रहा है. इसके कारण ये जिन छोटे-छोटे पौधों और जीवों को खाकर जिंदा रहते हैं, वो अपनी जगह बदल सकते हैं या खत्म हो सकते हैं.



.jpg)
.jpg)