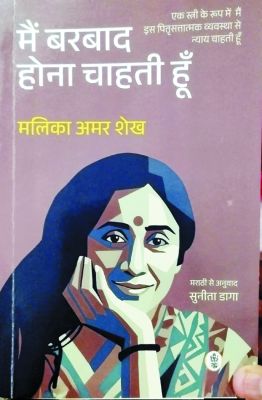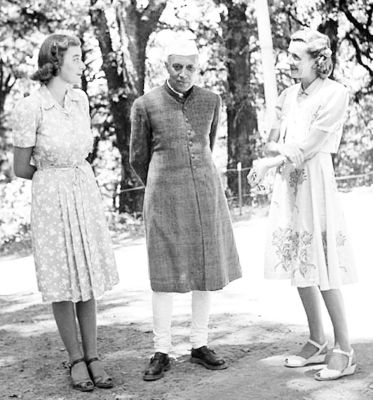विचार / लेख
जब पहली बार इंसान ने चांद पर कदम रखा था, उसके लगभग 60 साल बाद अब अंतरिक्ष एजेंसियां और निजी कंपनियां चांद से होते हुए मंगल पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं. लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है.
 डॉयचे वैले पर फ्रेड श्वालर का लिखा-
डॉयचे वैले पर फ्रेड श्वालर का लिखा-
सबसे पहले तो ये जान लीजिए:-
* अब इंसानों के लिए चंद्रमा पर जाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ईएसए मिलकर आर्टेमिस प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं।
* हाल में चीन और भारत ने कई सफल चंद्रमा मिशन पूरे किए हैं।
* अंतरिक्ष एजेंसियां और निजी कंपनियां अब चंद्रमा का इस्तेमाल वैज्ञानिक शोध और मंगल पर पहुंचने के लिए करना चाहती हैं।
चंद्रमा में बढ़ती दिलचस्पी
आर्टेमिस प्रोग्राम उत्तर अमेरिकी और नासा द्वारा संचालित एक मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। जिसमें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) सहित 55 अंतरराष्ट्रीय सहयोगी भाग ले रहे हैं।
चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक स्थायी बेस बनाना नासा का लक्ष्य है। जिसे ‘आर्टेमिस बेस कैंप’ कहा जाएगा। साथ ही, वह चंद्रमा की कक्षा में एक नया अंतरिक्ष स्टेशन ‘गेटवे’ भी लॉन्च करने की योजना बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ, चीन और रूस की साझेदारी में 13 अंतरराष्ट्रीय भागीदार साथ मिलकर एक चंद्र बेस बनाने की योजना बना रहे है, जिसे ‘इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन’ कहा जाएगा और इसे 2035 तक पूरा किये जाने की उम्मीद है।
आर्टेमिस बेस कैंप और इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन, दोनों को वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए बनाया जा रहा है। अगर यह योजनाएं सफल होती हैं, तो इनमें अंतरिक्ष यात्री कुछ समय के लिए रह सकेंगे और रोबोटिक उपकरणों को स्थायी रूप से वहां स्थापित किया जा सकेगा।
लेकिन चांद रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत रूस ने न केवल जमीन पर बल्कि अंतरिक्ष में भी अपना वैचारिक मतभेद जाहिर किया था। और आज के समय में भी ऐसा ही देखा जा रहा है। फर्क बस इतना है कि अब इसमें और भी देश शामिल हो चुके हैं। अमेरिका ने तो खुले तौर पर कहा ही है कि वह खुद को एक ‘स्पेस रेस’ में देखता है और उसे वह जीतना चाहता है।
इस दौड़ में जीतना काफी मायने रखता है क्योंकि:-चांद में बढ़ती दिलचस्पी का एक कारण यह भी है कि वह संसाधनों से भरपूर है। जैसे:-
* लोहा
* सिलिकॉन
* हाइड्रोजन
* टाइटेनियम
* दुर्लभ खनिज तत्व (रेयर अर्थ)
हालांकि, इन संसाधनों को निकालना और धरती तक लाना बहुत महंगा है। लेकिन धरती पर खनिजों के अभाव में उन्हें धरती पर लाया जा सकता है। अंतरिक्ष में छिपे विशाल खनिज भंडार, खासकर एस्टेरॉइड्स में मौजूद खजाने को हासिल करने की दिशा में चांद पर खनन की शुरुआत करना पहला कदम हो सकता है।
चांद से निकाले गए ज्यादातर संसाधनों का इस्तेमाल उन्हीं चीजों की जगह किया जाएगा, जिन्हें अब तक धरती से ले जाना पड़ता है। इससे चांद पर बनाए जाने वाले बेस की खनिजों के लिए धरती पर निर्भरता खत्म या ना के बराबर हो जाएगी।
उदाहरण के लिए, चंद्रमा की मिट्टी (रेगोलिथ) का उपयोग विकिरण (रेडिएशन) से सुरक्षा और चांद पर निर्माण कार्यों के लिए किया जा सकता है।
पानी, जिसकी खोज 2008 में भारत के चंद्रयान-1 मिशन ने की थी। उसका पीने, खाना उगाने और उपकरणों को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल हो सकेगा।
चंद्रयान-1 के बाद किए गए मिशनों ने दिखाया है कि चांद के ध्रुवों पर बर्फ की मात्रा काफी ज्यादा है। यही कारण है कि पहला चंद्र-बेस शायद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बनाए जाए सकता है। भले ही वहां उतरना चुनौतीपूर्ण हो।
इस बेस को मंगल पर जा रहे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ‘ट्रांजिट लाउंज’ यानी बीच के पड़ाव की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
ऊर्जा के लिए अभी कुछ अंतरिक्ष यान और सैटेलाइट सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रेगोलिथ और बर्फ का उपयोग रॉकेट के लिए ईंधन बनाने में भी किया जा सकता है।
चांद पर हीलियम-3 भी बड़ी मात्रा में पाया गया है, जो भविष्य में न्यूक्लियर फ्यूजन से बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसलिए, मंगल मिशन के लिए चांद पर रुकना और वहां से ईंधन भरना और जरूरी हो गया है।
चांद पर वैज्ञानिक शोध
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के ‘मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम’ की मैनेजर, सारा पास्टर ने डीडब्ल्यू को एक ईमेल में बताया कि चांद से जुड़े वैज्ञानिक शोध ईएसए के मिशन का मुख्य हिस्सा है। और यह बात बाकी अंतरिक्ष एजेंसियों पर भी लागू होती है।
पिछले 20 वर्षों से इंसान अंतरिक्ष में लगातार मौजूद रहा है, खासकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) पर। लेकिन आईएसएस धरती से सिर्फ 400 किलोमीटर (लगभग 250 मील) की दूरी पर है, जहां पहुंचने के लिए लॉन्च के बाद सिर्फ चार घंटे लगते हैं। इसके मुकाबले चांद धरती से चार लाख किलोमीटर (250,000 मील) दूर है, यानी वहां पहुंचने में लगभग तीन दिन लगते हैं। और यह सफर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कहीं ज्यादा जोखिम भरा होता है। इसलिए चांद पर शुरुआती रिसर्च का मकसद इस सफर को सुरक्षित और आसान बनाना होगा।
इसके बाद बात आती है पर्यावरण विज्ञान की। सारा पास्टर के अनुसार, ‘वैज्ञानिक यह पता लगाएंगे कि चांद का वातावरण कैसा है? उसके विशेष हालात इंसान के स्वास्थ्य पर क्या असर डालते हैं और रोबोटिक मिशनों पर क्या प्रभाव होता है। इसके अलावा इंसानी गतिविधियां चांद के पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती हैं।’
वैज्ञानिक यह भी जानना चाहते हैं कि चांद पर मौजूद पानी, धातु और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल लंबे समय तक चांद पर टिके रहने के लिए कैसे किया जा सकता है, और उन्हें सबसे प्रभावी तरीके से कैसे निकाला जा सकता है। सारा पास्टर ने बताया, ‘ईएसए, पर्यावरण के रेडिएशन को मापने वाले उपकरण, खुदाई और नमूना विश्लेषण, भूगर्भीय अध्ययन और अंतरिक्ष में चांद के मौसम को जांचने के लिए उपकरण विकसित कर रहा है।’
चांद की तकनीक धरती पर भी असरदार
अकसर ऐसा कहा जाता है कि मोबाइल फोन का श्रेय 1960 और 70 के दशक के अपोलो मिशनों को जाता है। हालांकि हमारे मोबाइल फोन सीधे तौर पर अंतरिक्ष तकनीक से नहीं आए हैं, लेकिन अपोलो मिशनों ने इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन उपकरणों को छोटा और हल्का बनाने में काफी मदद की थी।
अंतरिक्ष एजेंसियों के रिसर्च और डेवलपमेंट लैब्स में तैयार की गई कई आधुनिक तकनीक आज धरती पर लोगों के जीवन को बेहतर बना रही हैं। जैसे कि घरों में की जाने वाली इंसुलेशन यानी अत्यधिक गर्मी या सर्दी से बचाने वाली परत, गद्दों में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी फोम, खाने को सुखाने और जमाने की तकनीक, रोबोटिक सेंसर्स और टेलीमेडिसिन यानी दूर से इलाज करने की तकनीक इत्यादि।
वैज्ञानिक ऐसे मेडिकल उपकरण और स्वास्थ्य निगरानी के तरीके विकसित कर रहे हैं, जो अंतरिक्ष के बेहद कठिन हालातों में लंबे समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के बीच सेहत की रक्षा कर सकें। खासकर उनकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि ऐसे हल्के और पोर्टेबल डायग्नोस्टिक उपकरण बनाना, जो बिना मेडिकल ट्रेनिंग वाले स्पेस क्रू को भी अपनी सेहत की निगरानी में मदद कर सकें।
इन तकनीकों का इस्तेमाल भविष्य में धरती पर भी किया जा सकता है।
क्या मंगल इंसानों का दूसरा (या तीसरा) घर बन सकता है?
चांद की सतह और उसकी कक्षा में स्थायी बेस बनाने का लक्ष्य यही रहा है कि उसे अंतरिक्ष में जाने के लिए एक ठहराव या पड़ाव के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।
सारा पास्टर के अनुसार, ‘चांद पर एक कॉलोनी बनाना बेहद उपयोगी होगा और यह मंगल ग्रह की सतह पर इंसानों को भेजने के लिए एक अहम प्रशिक्षण स्थल भी बन सकेगा।’
अमेरिकी अंतरिक्ष एवं अनुसंधान एजेंसी नासा 2030 के दशक में ही अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल पर भेजना चाहती है। (dw.com/hi)