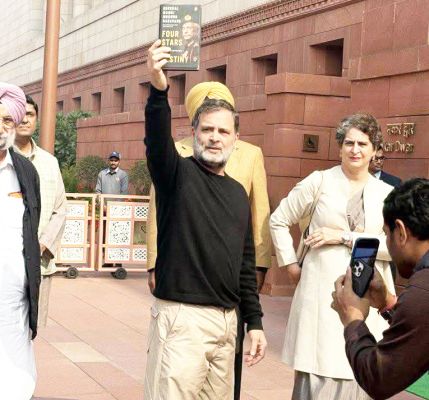विचार / लेख

-डॉ. संजय शुक्ला
पाकिस्तान के लाहौर से एक खबर आई कि वायु प्रदूषण के चलते एक ही दिन में 75 हजार बीमार अस्पताल पहुंचे। इस खबर में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान के लगभग 1.4 करोड़ लोग सांस की संकट से जूझ रहे हैं।गौरतलब है कि स्वीटजरलैंड की संस्था आईक्यू एयर की ‘वल्र्ड एयर क्वालिटी-2024’ रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में बांग्लादेश, पाकिस्तान के बाद भारत तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है।
रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर पाकिस्तान का लाहौर है तथा प्रदूषित शहरों में से 83 शहर भारत के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित राजधानियों में नई दिल्ली दूसरे पायदान पर रहा। आंकड़ों को देखें तो देश के 60 फीसदी शहरों में प्रदूषण का स्तर डब्ल्यूएचओ के मानक से सात गुना ज्यादा है। ‘विंटर सीजन’ यानि सर्दियों के मौसम को ‘हेल्दी सीजन’ कहा जाता है लेकिन दिल्ली-एनसीआर सहित देश के विभिन्न शहरों में यह मौसम लोगों के सेहत के लिए मुसीबत लेकर आता है। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर से कहर बरपाने लगा है तथा सरकार और प्रशासन हांफने लगी है। दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित दूसरे राजधानी दिल्ली की बात करें तो हालिया आफत कोई पहली बार नहीं आई है अपितु अमूमन हर साल अक्टूबर से लेकर पूरे सर्दियों के मौसम में दिल्ली वासियों पर वायु प्रदूषण का कहर बरपता है। इस दौरान समूचा दिल्ली -एनसीआर का इलाका धुंध यानि स्मॉग से लिपटी हुई है तथा यह महानगर ‘गैस चैंबर’के रूप में तब्दील हो चुका है।
आलम यह है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से उड़ान भरने वाले घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमानों को निम्न दृश्यता की वजह से विलंबित करना पड़ रहा है अथवा उनका रूट बदलना पड़ रहा है। संभवतया आने वाले समय में दिल्ली के ट्रैफिक पर दबाव कम करने के लिए ऑड-इवन व्यवस्था लागू करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जहरीली होती हवा के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। अलबत्ता यह पहली मर्तबा नहीं है जब दिल्ली की दमघोंटू हवा पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई हो लेकिन केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और प्रशासन पर इसका कोई असर दृष्टिगोचर नहीं होता।
सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ‘सफर-इंडिया’ के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में द्वारका, मुंडका तथा नजफगढ़ जैसे इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानि एक्यूआई 500 दर्ज किया गया। पिछले साल भी इसी सीजन में दिल्ली में एक्यूआ?ई का स्तर 500 तक पहुंच गया था जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ‘ड्ब्ल्यूएचओ’ के तय मानक से 100 गुना ज्यादा है। मानकों के मुताबिक 0-50 अच्छा,51-100 संतोषजनक, 101-200 मध्यम, 201-300 खराब,301-400 बहुत खराब और 401 से 500 एक्यूआई को गंभीर श्रेणी में माना जाता है।
बहरहाल सिर्फ भारत की राजधानी दिल्ली की हवा ही दमघोंटू नहीं है बल्कि दिल्ली से सटे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तरप्रदेश सहित देश के अनेक बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर खराब से बहुत खराब स्तर पर है। दिल्ली सरकार जहाँ प्रदूषण की वजह दिल्ली से सटे राज्यों के किसानों द्वारा पराली जलाने को बताती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस दलील पर नाइत्तेफाकी जाहिर करते हुए दिल्ली के नौकरशाही को उसकी निष्क्रियता पर फटकार लगाया था। दिल्ली सहित उत्तर भारतीय राज्यों में हर साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले भयावह प्रदूषण के लिए पराली जलाने की वजह को नकारा नहीं जा सकता लेकिन इसके लिए उद्योगों व वाहनों के धुआं उत्सर्जन और सडक़ों तथा निर्माण स्थलों से उडऩे वाला धूल भी काफी हद तक जवाबदेह है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ‘डब्ल्यूएचओ’ द्वारा दुनिया के 1650 शहरों वायु प्रदूषण पर में किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक भारत की राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अन्य शहरों की तुलना में बहुत खराब है। बहरहाल भारत जैसे विकासशील देश में वायु प्रदूषण बहुत ही गंभीर चुनौती है जिसका असर जनस्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन 70 लाख असामयिक मौतें होती हैं,जिसमें अकेले भारत में 20 लाख लोगों की मौत होती है। एक अन्य शोध के मुताबिक भारत में प्रदूषण के कारण लोगों की जिंदगी पांच साल कम हो रही है। प्रदूषण के कहर से लाखों लोग फेफड़ों और दिल के गंभीर बीमारियों का शिकार भी होते हैं।
आलम यह कि देश के सैकड़ों शहरों की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में हैं फलस्वरूप बच्चों और बुजुर्गों में श्वसन तंत्र से संबंधित रोगों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके अलावा कैंसर, मधुमेह, स्ट्रोक, फेफड़ों के कैंसर और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ‘सीओपीडी’ जैसे रोगों का एक मुख्य वजह वायु प्रदूषण है। पर्यावरण प्रदूषण से केवल जनस्वास्थ्य पर ही बुरा असर नहीं पड़ रहा है बल्कि इसका अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ रहा है जिससे देश की आर्थिक और सामाजिक विकास बाधित हो रही है।
वायु प्रदूषण के कहर से छत्तीसगढ़ राज्य भी अछूता नहीं है, इस राज्य के औद्योगिक शहर जहाँ कोयला आधारित उद्योग और निर्माण कार्य संचालित हो रहे हैं वहां वायु प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राज्य के राजधानी रायपुर सहित सभी प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता को संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता वहीं घरों के छतों और फर्श पर काली धूल की परत वायु प्रदूषण की चुगली कर रहा है।
औद्योगिक नगरी कोरबा के रहवासी अब सफेद राखड़ और काली धूल के आदी हो चुके हैं वहीं रायगढ़, भिलाई सहित अन्य शहर कोयला आधारित उद्योगों से निकलने वाले धुआं और धूल की वजह से हलाकान हैं। छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भी किसान अब अगली फसल के लिए खेतों में पराली जलाने लगे हैं जो भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय बन सकता है।
राज्य में औद्योगिक प्रदूषण के कारण आसपास के गांवों के खेत बंजर में तब्दील हो चुके हैं फलस्वरूप कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है। वायु प्रदूषण सिर्फ आम जनजीवन को ही प्रभावित नहीं कर रहा है बल्कि यह पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं सहित परिस्थिकीय तंत्र पर भी बुरा असर डाल रहा है।
देश में प्रदूषण के लिए मुख्यतौर से बढ़ती आबादी, पराली जलाने, कारखानों और वाहनों के धुएं, पटाखों और निर्माण स्थलों से उडऩे वाले धूल, खाना पकाने के लिए चारकोल और लकड़ी का उपयोग, जंगलों की अंधाधुंध कटाई और खनिज खनन सहित एयरकंडीशनर का बढ़ता उपयोग इत्यादि कारण जिम्मेदार हैं। भारत एक उत्सवधर्मी देश है जहां दीपावली सहित विभिन्न उत्सवों में खूब पटाखे छोड़े जाते हैं। बिलाशक पटाखों से वायु और ध्वनि प्रदूषण दोनों होता है लेकिन सरकारी बंदिश को धता बताकर खूब पटाखे जलाए और छोड़े जाते हैं।
पटाखों में तांबा, कैडमियम, सल्फर, एल्यूमिनियम, बेरियम, आर्सेनिक, लीथियम के घातक रासायनिक कंपाउंड होते हैं जिसके जलने से जहरीला धुआं निकलता है। इस धुआं की वजह से सांस संबंधी रोग, त्वचा और नेत्ररोग सहित फेफड़ों के कैंसर हो सकता है।
पटाखों के तेज आवाज की वजह से श्रवण शक्ति कमजोर हो सकती है इसके अलावा हृदय से संबंधित विभिन्न रोग, हृदयाघात, उच्च रक्तचाप और अनिद्रा जैसे रोग भी हो सकते हैं। पटाखों से निकलने वाली धुआं और तेज आवाज पर्यावरण और परिस्थितिकी तंत्र पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। घातक धुआं और आवाज पेड़-पौधों और पालतू पशुओं पर भी बुरा असर डालते हैं। आसन्न दीपावली के मद्देनजर यह भी तय है कि तमाम पाबंदियों और खतरों के बावजूद पटाखे तो चलेंगे लेकिन इस दिशा में आम नागरिकों की भी जवाबदेही है कि वे सेहत और पर्यावरण के लिहाज से ग्रीन पटाखों का उपयोग करें।
अलबत्ता देश की सरकारें और आम जनता पर्यावरण प्रदूषण के प्रति कितना गंभीर है? इसका अंदाजा सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, विक्रय और उपयोग संबंधी प्रतिबंधात्मक कानून से पता चलता है।गौरतलब है कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने 1 जुलाई 2022 से देश में एक बार उपयोग लायक ‘सिंगल यूज प्लास्टिक’ के आयात, निर्माण, भंडारण, विक्रय और उपयोग को प्रतिबंधित करने का अधिसूचना जारी किया था। राज्य सरकार ने भी इस दिशा में फौरी सख्ती दिखाई थी लेकिन आज भी इन चीजों का निर्माण, बिक्री और उपयोग धड़ल्ले से जारी है। दरअसल सिंगल यूज प्लास्टिक नॉन-बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो सैकड़ों सालों तक नष्ट नहीं होते। कचरों के साथ प्लास्टिक के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और डाई-ऑक्सीन जैसी जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है जो मनुष्य के श्वसन और तंत्रिका तंत्र को बहुत नुकसान पहुंचाता है साथ ही यह गर्भवती माता और गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी घातक होता है। एक वैज्ञानिक शोध के मुताबिक सिंगल यूज प्लास्टिक के जलने से पैदा होने वाले धुएं से फेफड़े से संबंधित दमा, टीबी और कैंसर सहित आंखों से संबंधित रोग हो सकते हैं।
गौरतलब है कि साल दर साल बढ़ते जानलेवा प्रदूषण का असर भारत जैसे गरीब देशों के लोगों के सेहत के साथ-साथ घरेलू बजट और आजीविका पर भी पडऩा अवश्यंभावी है इसलिए इस समस्या के प्रभावी समाधान के प्रति सचेत होना जरूरी है।देश में पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो सरकारों के कथनी और करनी में काफी विरोधाभास है तो आम नागरिक भी इस दिशा में काफी लापरवाह हैं। सरकार और समाज ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के नाम पर हर साल 5 जून को ‘विश्व पर्यावरण दिवस’ अवसर पर रस्मी आयोजनों में शाब्दिक जुगाली कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेता है। एक शोध के मुताबिक अगर इसी तरह वायु प्रदूषण बढ़ता रहा तो सन 2050 तक पृथ्वी 4 से 5 डिग्री तक गर्म हो जाएगी।
दूसरी ओर विभिन्न रिपोर्ट यह बताते हैं कि भारत प्रदूषण को लेकर तनिक भी गंभीर नहीं है बल्कि इस विकराल समस्या पर हम सिर्फ जुबानी जमा खर्च ही कर रहे हैं। दुखदाई यह कि यदि हम अब भी नहीं चेते तो आने वाले समय में इसकी कीमत भावी पीढ़ी को चुकानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि देश में प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी कानून नहीं है लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति के आभाव और विभागीय अमले की उदासीनता के कारण तमाम कानून किताबों में ही कैद हैं।यह कटु सत्य है कि देश में बढ़ रहे विभिन्न प्रदूषणों के लिए जहां सरकार की पर्यावरण विरोधी नीतियां जिम्मेदार हैं वहीं इस समस्या के लिए आम नागरिक भी पूरी तरह से जवाबदेह हैं।
विचारणीय है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है लेकिन इस देश में पर्यावरण कभी भी राजनीतिक या चुनावी मुद्दा नहीं बना।दिल्ली में जहरीली हवा पर हर साल मचने वाले सियासी बवाल को परे रख दें पर्यावरण प्रदूषण कभी भी संसद में गंभीर बहस का मुद्दा नहीं बना।अलबत्ता जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए प्रदूषण पर प्रभावी रोकथाम जरूरी है, इसके लिए जंगलों की कटाई, कोयला खनन, पहाड़ों की कटाई व खुदाई को रोकते हुए औद्योगिक व अधोसंरचनात्मक प्रदूषण पर सख्ती से रोकथाम लगाना होगा लेकिन सरकारों के औद्योगिक और चकाचौंध विकास की भूख इसमें बाधक हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को सीमित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और बॉयोगैस के प्रचलन को प्रोत्साहित करना होगा वहीं अपरंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना होगा। आम नागरिकों की भी जवाबदेही है कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए लागू प्रतिबंधों और कानूनों के प्रति स्व-अनुशासित और जागरूक हों।