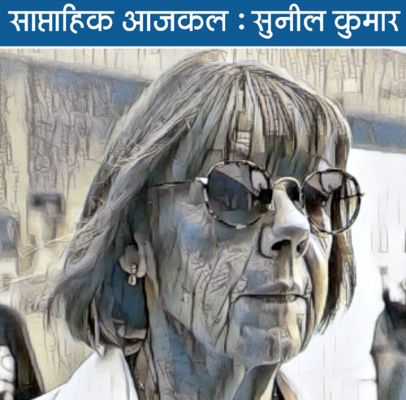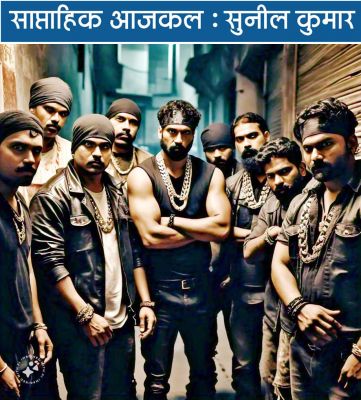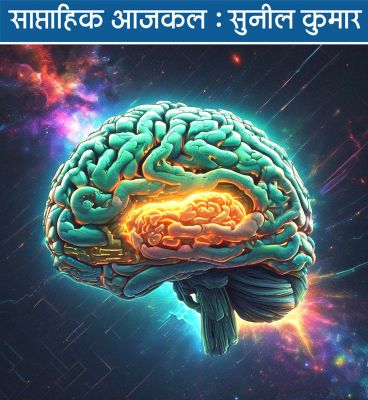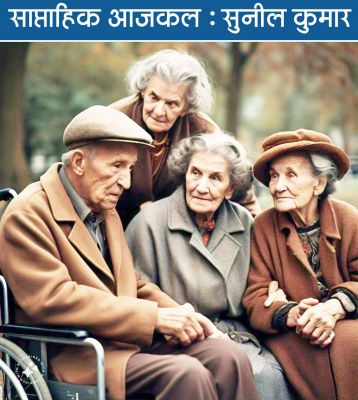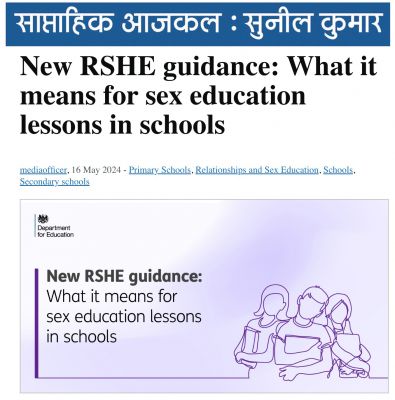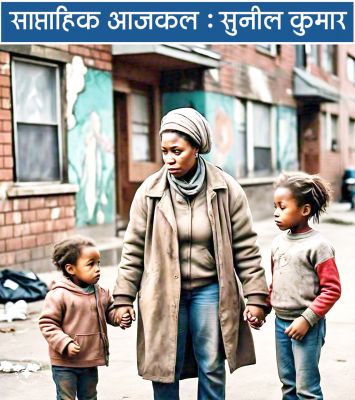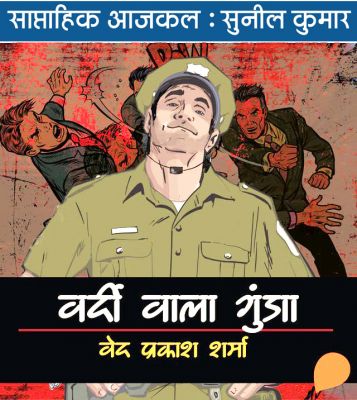आजकल
मुम्बई हिन्दुस्तान की कारोबारी राजधानी है, और जाहिर है कि कमाई या कारोबारी ताकत के लिए होने वाले जुर्म यहां पर देश के दूसरे शहरों के मुकाबले कुछ अधिक होते होंगे, लेकिन जब इस महानगर में धमकी देकर किसी प्रमुख व्यक्ति का कत्ल कर दिया जाता है, तो यह राज्य सरकार और स्थानीय पुलिस की एक बड़ी नाकामयाबी तो रहती ही है। पूरी जिंदगी कांग्रेस के एक प्रमुख नेता रहे हुए बाबा सिद्दीकी जिस इलाके के पार्षद और विधायक निर्वाचित होते रहे, वहां पर बसे फिल्म उद्योग के लोगों की वजह से उनके चर्चित फिल्मकारों से करीबी रिश्ते रहे। वे कई बार विधायक रहे, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे, और पिछले एक पखवाड़े से वे कत्ल की धमकी के साए में, और सरकार की मुहैया कराई गई वाई केटेगरी की सुरक्षा के घेरे में चल रहे थे। ऐसे में जाहिर धमकी, और जाहिर खतरे को देखते हुए भी अगर पुलिस उन्हें नहीं बचा पाई, तो यह सरकार पर एक बड़ा सवालिया निशान भी बनता है। हाल ही में वे जिंदगी भर की कांग्रेस को छोडक़र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आए थे, और वे फिल्म अभिनेता सलमान खान के बहुत करीबी माने जाते थे जिन्हें मारने की घोषणा जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई नाम के एक बड़े गैंगस्टर ने की हुई है। अब यह भी माना जा रहा है कि यह कत्ल इसी गिरोह के लोगों ने भाड़े के हत्यारों से करवाया है, और अभी गिरफ्तार दो लोगों को कहा जाता है कि इसी गिरोह ने 50-50 हजार रूपए दिए थे।
अब अगर चार लोगों को 50-50 हजार रूपए देकर कुल दो लाख रूपए में मुम्बई में वाई केटेगरी की सुरक्षा से घिरे हुए व्यक्ति का कत्ल करवाया जा सकता है, तो फिर इस देश में किसे सुरक्षित समझा जा सकता है? पुलिस ने तीन हमलावरों में से दो को पकड़ा है, और उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का नाम लिया है। देश में कई और चर्चित कत्ल इसी गैंगस्टर ने जेल में रहते हुए करवाए हैं, और उनका दावा भी किया है, जिम्मेदारी भी ली है। खबरें तो ऐसी भी हैं कि यह देश के बाहर भी कत्ल करवाता है। मुम्बई में अपने इलाके में 30 बरस से अधिक की राजनीति वाले लोकप्रिय और ताकतवर राजनेता को अगर दो लाख रूपए में मरवाया जा सकता है, तो फिर बाकी लोगों को अपने बारे में सोच लेना चाहिए।
पिछले कई बरस से देश में लगातार यह देखने मिलता है कि लाख-पचास हजार रूपए में भाड़े के हत्यारे जुटाए जा सकते हैं, और लाख-दो लाख रूपए में कारखाने में बनी हुई असली पिस्तौल या रिवॉल्वर जुटाई जा सकती है। देश के बहुत से प्रदेशों में ठेके पर ऐसी सुपारी-हत्या होती है, और हत्यारों की कोई कमी नहीं दिखती है। क्या सिर्फ बेरोजगारी की वजह से नौजवान ऐसी सुपारी उठाते हैं, और कत्ल करते हैं? या फिर उन्हें जुर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए दाऊद इब्राहिम या लॉरेंस बिश्नोई की तरह का बड़ा गैंगस्टर बनने की हसरत रहती है जो कि जेल के भीतर से, या दूसरे देश से भी जुर्म की अपनी दुनिया चलाते दिखते हैं?
महानगर मुम्बई जहां पर कि देश की सबसे अधिक ताकतवर पुलिस तैनात मानी जाती है में जितने में यह कत्ल हुआ है, उतने में तो पैसेवालों की एक बर्थडे पार्टी नहीं होती। और गैंगस्टरों का हाल यह है कि वे देश में सबसे कड़ी हिफाजत वाली जेलों के भीतर से भी तरह-तरह के मोबाइल से अपना साम्राज्य चलाते हैं। अब अगर देश की राजधानी की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल के भीतर से अगर गैंगस्टर धमकी देकर रकम मांगे, और हर कुछ महीनों में उसके करवाए चर्चित कत्ल सामने आते रहें, तो फिर किसकी यह ताकत है कि वह मुंहमांगी रकम दिए बिना चैन की नींद सो सके? महाराष्ट्र सरकार और मुम्बई पुलिस से जिसे वाई केटेगरी की हिफाजत मिली हुई हो, उसके ऐसे कत्ल के बाद तो किसी गैंगस्टर को जेल के भीतर से फोन करके धमकाने की जरूरत भी नहीं है। देश के दौलतमंद लोगों के सामने आज तो यह बात एकदम साफ है कि सरकारी इंतजाम शायद ही किसी को बचा सके। यह भी हो सकता है कि आज अनगिनत दौलतमंद लोग पुलिस को बताए बिना, अघोषित रूप से गैंगस्टरों को पैसा देते हों, जैसा कि एक वक्त मुम्बई में दाऊद इब्राहिम की तरफ से वसूला जाता था।
हम लाख-पचास हजार रूपए भाड़े वाले कातिलों की बात नहीं करते, वे तो बेरोजगार नौजवान हो सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से सरकारों के तहत आने वाली जेलों को देखकर हैरान हैं कि वहां मुजरिमों का राज इस हद तक चलता है। सरकारों की बड़ी नाकामयाबी सडक़ पर कत्ल नहीं है, जेलों से कत्ल का हुक्म देना है। अब इसे क्या कहा जाए कि देश की राजधानी में दुनिया की एक सबसे बड़ी जेल, तिहाड़ जेल में जहां करीब 20 हजार कैदी हैं, और जिसे देश में सबसे अधिक हिफाजत की जेल माना जाता है, जो चार सौ एकड़ जमीन पर फैली हुई है, वहां देश के सबसे खूंखार और ताकतवर गैंगस्टर राज कर रहे हैं। यह बात दिल्ली सरकार के लिए शर्मिंदगी की है, या इस सरकार पर राज करने वाले, केन्द्र सरकार से नियुक्त एलजी के लिए शर्मिंदगी की होनी चाहिए?
हिन्दुस्तान में अरबपतियों की गिनती बढ़ती चल रही है। दूसरी तरफ सार्वजनिक जीवन के फिल्मी सितारों, खिलाडिय़ों, और चर्चित लोगों की कोई कमी तो है नहीं। झारखंड के एक गिरोह के शूटर कुछ हफ्ते पहले छत्तीसगढ़ में करोड़ों की वसूली के लिए धमकी देने के बाद आकर एक कारोबारी के दफ्तर पर गोलियां चला गए हैं। नेताओं से लेकर कारोबारियों तक ऐसा हर कत्ल देश के अलग-अलग दायरों में अस्थिरता लेकर आएगा, इनसे महज एक-एक जिंदगी खत्म नहीं होगी, इनसे बहुत सी और उथल-पुथल होगी। देश-प्रदेश की सरकारों को इस खतरे को समझना चाहिए। लेकिन सरकारों के साथ हमारी यह हमदर्दी भी है कि जहां लाख-पचास हजार में किसी के भी कत्ल की सुपारी दी जा सकती है, वहां करोड़ों बेरोजगारों को इस धंधे से कैसे बचाया जा सकेगा? (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
एक महिला डॉक्टर से सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बलात्कार और उसकी हत्या से उबला और बिफरा हुआ बंगाल कल फिर सुलग गया जब दस साल की एक बच्ची की लाश मिली। उसके गायब होने की शिकायत पुलिस में दर्ज थी लेकिन पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए गांव की भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, और वहां खड़ी गाडिय़ों को भी। इसी के साथ दूसरी खबर गुजरात की है। वहां एक नाबालिग लडक़ी से उसके दोस्त की मौजूदगी में ही दो लोगों ने वडोदरा शहर के बाहरी हिस्से में बलात्कार किया। जिस वक्त गुजरात में चल रहे विख्यात सालाना गरबा महोत्सव के आने-जाने वाले लोगों की भीड़ पूरी रात सडक़ों पर रहती है। ये दोनों स्कूटी पर आ रहे थे, और आधी रात के करीब दो दोपहियों पर पांच लोगों ने उन्हें रोका, और इनमें से एक ने लडक़े को पकडक़र रखा, और दो ने इस लडक़ी से बलात्कार किया। इसी रात महाराष्ट्र में पुणे शहर के किनारे पर अपने दोस्त के साथ जा रही एक युवती से तीन अनजान लोगों ने बलात्कार किया। उन्होंने इस पुरूष-दोस्त को उसके कपड़ों और बेल्ट से बांधकर घायल भी कर दिया था।
अब बंगाल की घटना तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता के राज की है, गुजरात की घटना भाजपा शासन की है, और महाराष्ट्र घटना भाजपा गठबंधन सरकार की है। इसलिए ये घटनाएं अभी अधिक बड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं बन रही हैं, कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर। एक वजह यह भी हो सकती है कि मध्यप्रदेश में हरदा जिले की महिला कांग्रेस अध्यक्ष के पति ने शादी का झांसा देकर एक युवती से कई बार बलात्कार किया, और उसकी रिपोर्ट पर अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी ही खबरों को देखें तो दो दिन पहले यूपी में समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव, और उनके छोटे भाई जुगेन्द्र समेत चार लोगों पर 9 साल बाद बलात्कार का जुर्म दर्ज हुआ है। इन दोनों भाईयों के खिलाफ पहले से डेढ़ सौ से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, दोनों अभी अलग-अलग जेलों में दूसरे जुर्मों में बंद हैं, और इनके खिलाफ बलात्कार के भी कई मामले दो बरसों में दर्ज हुए हैं। याद रखने की बात यह है कि 2017 से यूपी में भाजपा के योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और उनके राज में बलात्कार की खबरें आना कभी थमी नहीं हैं।
भारत के बारे में पूरी दुनिया में यह तस्वीर बनी हुई है कि यहां कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। और इस बात को देश पर सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ इसलिए नहीं माना जाना चाहिए कि दिल्ली जैसे एक राज्य को छोडक़र बाकी तमाम राज्यों में तो अलग-अलग पार्टियों की सरकारें हैं, और सिर्फ दिल्ली में ही पुलिस केन्द्र सरकार के मातहत है। बाकी राज्यों में तो वहां की स्थानीय सरकारें पुलिस महकमा चलाती हैं, और जुर्म, कानून-व्यवस्था जैसे मामले प्रदेश सरकार के जिम्मे ही आते हैं। इसलिए देश के बाहर अगर भारत की इस बात को लेकर बदनामी है कि यहां कोई महिला या लडक़ी सेक्स-अपराधों के खतरे से परे नहीं हैं, तो इसे केन्द्र सरकार को अपनी बदनामी नहीं मानना चाहिए।
इस देश में बलात्कार सिर्फ आज की लडक़ों या मर्दों की उत्तेजना का नतीजा नहीं है, इसके पीछे भारतीय समाज की सदियों की सोच भी जिम्मेदार है, और समाज का आज का यह पाखंड भी जिम्मेदार है कि लडक़े-लड़कियों को मिलने-जुलने नहीं देना। जब किशोरावस्था के बाद जवान लडक़े-लड़कियों की देह तैयार हो जाती है, जब उनके तन-मन की जरूरतें बढ़ जाती हैं, तब भी उनका आपस में मिलना सामाजिक हिकारत का शिकार होता है, और उन्हें किसी होटल के बंद कमरे में मिलना जुर्म जैसे साए तले हो पाता है। एक स्वाभाविक हमउम्र प्यार को, सेक्स की जरूरत को, भारत में जिस तरह अनदेखा किया जाता है, उसके पीछे यह सामाजिक सोच भी है कि प्यार और सेक्स शादी के बाद की चीजें हैं। इस तरह जब प्यार और सेक्स को अवांछित करार दिया जाता है, तो लोग कम से कम सेक्स को पाने के लिए जुर्म करने को भी तैयार हो जाते हैं। भारत में सेक्सकर्मियों के कारोबार को कानूनी मान्यता नहीं है। इसलिए जिनके दिमाग पर सेक्स सवार रहता है, जो हिंसा की हद तक जाकर बलात्कार को भी तैयार हो जाते हैं, उनके पास पैसे खर्च करके सेक्स पाने का कोई आसान विकल्प नहीं रहता है। सेक्स कारोबार भारत में अभी भी जुर्म सरीखा है, और नतीजा यह होता है कि सेक्स-कुंठा के शिकार लोग आसपास के बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं।
दूसरी बात सामाजिक स्थिति की है, परिवारों के भीतर लड़कियों और महिलाओं को परिवारों के ही बड़े आदमियों की हिकारत और हिंसा का शिकार देखते हुए बड़े होने वाले बच्चे वैसी ही मानसिकता लेकर बालिग होते हैं। उन्हें यही समझ रहती है कि लड़कियां और महिलाएं बलात्कार के लायक हैं, हिंसा के लायक हैं। नतीजा यह होता है कि ऐसे नौजवान, अधेड़ और बूढ़े हो जाने पर भी ऐसी हिंसा को अपना हक मानते हैं, और परिवार में, समाज-व्यवस्था में, जाति-व्यवस्था में, आर्थिक पैमानों पर अपने से कमजोर लडक़ी या महिला को बलात्कार का सामान मानकर चलते हैं। दूसरी तरफ हमने यह देखा है कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष जिस डंके की चोट पर संसद में भी बने रहे, और बहुत लंबे समय तक इस महासंघ पर भी काबिज रहे, भाजपा में भी बने रहे, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही दिल्ली पुलिस ने इस बाहुबली नेता के खिलाफ जुर्म दर्ज करके जांच शुरू की थी। इसलिए जब दुनिया की यह सबसे बड़ी संसद, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने देह-शोषण के आरोपी को किसी कार्रवाई के लायक नहीं पाते, तो फिर यह बात एक मिसाल बनकर सब पर लागू हो जाती है, हर किसी का हौसला बढ़ा देती है।
लोकतंत्र सिर्फ अदालत से चलने वाली व्यवस्था नहीं हो सकती कि किसी प्रदेश में होने वाले सबसे चर्चित बलात्कार की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए, और उसकी निगरानी में कई तरह के हुक्म हो, और उससे देश सुधर जाए। देश को चलाने का सबसे बड़ा जिम्मा राजनीतिक दलों के नेताओं की अगुवाई में चलने वाली सरकारों का है। लोकतंत्र के दो और स्तंभों, विधायिका, और न्यायपालिका की भूमिकाएं सरकार के मुकाबले कम दखल की रहती हैं। और आज इन दोनों की कोई दिलचस्पी देश में बलात्कार घटाने में नहीं है, बल्कि सिर्फ इसमें है कि किस तरह अपने करीबी बलात्कारियों को बचाया जाए, और विरोधियों के करीबी बलात्कारियों के खिलाफ जुलूस निकाले जाएं।
देश की जिस संसद को बलात्कार घटाने के लिए एक गंभीर चर्चा करनी थी, वह इतनी भयानक गुटबाजी में फंसी हुई है, उसमें सत्ता और विपक्ष के गठबंधनों का इतना मजबूत ध्रुवीकरण है कि वहां पर किसी तरह की उन्मुक्त चर्चा मुमकिन ही नहीं है। बल्कि संसद के हाल को देखें तो ऐसा लगता है कि इस देश में किसी संसदीय बहस की जरूरत नहीं है, और अलग-अलग राजनीतिक दलों के कोई एक प्रतिनिधि भी अपनी सांसद-संख्या के मुताबिक वोट डाल दें, वही काफी होगा, किसी चर्चा की जरूरत ही क्या है? यह नौबत इस देश में बलात्कार के पीछे की सामाजिक हकीकत पर, कानूनी कमजोरियों पर कभी गंभीर चर्चा नहीं होने देगी, और बलात्कार को महज एक पुलिस और अदालत का मामला मानकर यह देश कभी इस हिंसा पर काबू नहीं पा सकेगा। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
हिन्दुस्तान की हिन्दू संस्कृति में पति-पत्नी के साथ को सात जन्मों का माना जाता है। खैर, सात किसने देखे हैं, एक जन्म भी साथ निभ जाए, तो काफी होता है। लेकिन दुनिया की कुछ दूसरी संस्कृतियों में भी पति-पत्नी अपने साथ को उजागर करने के लिए हाथ की किसी खास उंगली में अंगूठी पहनते हैं, और यह उनके किसी जीवनसाथी की तरफ ठीक वैसा ही इशारा होता है जैसा कि भारत में हिन्दू महिलाओं के गले में मंगलसूत्र, या उनकी मांग में सिंदूर से उजागर होता है। पश्चिम की, भारत में बदनाम, संस्कृति में भी कई मर्द ऐसे होते हैं जो बीवी के गुजर जाने के बाद भी ऐसी अंगूठी पहने रहते हैं, और यह उजागर करता है कि वे किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं।
एक खबर बेंगलुरू की है कि वहां पति को छोडक़र अलग रहने वाली महालक्ष्मी नाम की 29 बरस की एक महिला का ओडिशा के एक आदमी से प्रेमसंबंध हो गया था, और दोनों के बीच बहस होने पर उसने महालक्ष्मी का कत्ल करके उसके 59 टुकड़े कर दिए, और उन्हें फ्रिज में भरकर चले गया। बाद में जब इस फ्लैट से बदबू बाहर निकलने लगी, तो लोगों ने पुलिस को खबर की, और उसे लाश के टुकड़े मिले, पता लगाते हुए वह कातिल तक पहुंची, लेकिन उसे पुलिस की खबर लगने पर उसने जुर्म कुबूल की चिट्ठी लिखकर खुदकुशी कर ली। अब यह तो बिना किसी पश्चिमी प्रभाव वाला खालिस हिन्दुस्तानी मामला है जिसमें प्रेम या देहसंबंध से शुरूआत होकर कातिल और लाश तक संबंध पहुंच गया था। बात-बात में पश्चिम को कोसना पूरब की अपनी दिक्कतों का कोई हल नहीं होता।
ऐसे ही पश्चिम के एक देश फ्रांस से अभी एक खबर आई जो स्तब्ध कर देने वाली है। वहां अदालत ने 71 बरस के एक आदमी पर यह मुकदमा चल रहा था कि वह अपनी बीवी को दवाईयों से बेसुध कर देता था, और उसके बाद इंटरनेट पर पहले से छांटे गए लोगों को न्यौता देकर बुलाकर रखता था, और अपनी पत्नी पर उनसे बलात्कार करवाता था। ऐसे 50 लोगों पर यह मुकदमा चल रहा था जिन्होंने पति के बुलावे पर आकर बेसुध पत्नी के साथ सेक्स किया था। इनमें से कुछ लोगों को इस पति ने यह भरोसा दिलाया था कि पत्नी खुद ऐसा सेक्स चाहती है, और वह बेसुध होने का नाटक कर रही है। नौ बरस चले इस मुकदमे में आखिर में 71 बरस के इस आदमी ने यह माना कि वह बलात्कारी है, और उसी की तरह जो 50 दूसरे लोग इस अदालत में मौजूद हैं, वे भी बलात्कारी हैं। उसने अपनी पत्नी, बच्चों, और उनके भी बच्चों से माफी मांगते हुए कहा कि उसका यह जुर्म माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन उसे अफसोस है। उसने अदालत में मौजूद 50 आरोपियों के बारे में कहा कि उन सबको यह मालूम था कि वह उन्हें अपनी पत्नी से बलात्कार करने के लिए बुला रहा है।
फ्रांस में चला यह मुकदमा अपने आपमें दुनिया का अनोखा मुकदमा है जिसमें किसी आदमी ने अपनी पत्नी से ऐसे बलात्कार करवाए, और फिर उसके फोटो और वीडियो भी लेकर रखे थे जिनसे जांच अधिकारी इन आमंत्रित बलात्कारियों तक पहुंच पाए। इस पत्नी ने दस बरस तक चले ऐसे बलात्कारों से नावाकिफ रहते हुए अदालत में यही कहा कि उसके लिए यह कल्पना भी मुश्किल थी कि उसका पति उसके साथ ऐसा कर सकता है। उसने पल भर भी ऐसा नहीं सोचा, और उसे पति पर पूरा भरोसा था। अदालत में जब जांच अफसरों ने इस पत्नी को बलात्कार की ये तस्वीरें दिखाईं जो उसके पति ने ही खींची हुई थीं, तो वह हक्का-बक्का रह गई। यह शादी 20 बरस के आसपास की उम्र में हुई थी, और पत्नी आखिरी दिन तक यह मानकर चल रही थी कि उनकी शादी मजबूत है। आसपास के लोग भी उन्हें एक आदर्श जोड़ा मानते थे। लेकिन 2011 से इस पति ने अपनी इस खूंखार कल्पना को शक्ल देना शुरू कर दिया था, और वह नींद की गोलियां पीसकर पत्नी के खाने और पीने में मिला देता था, और जब वह बेहोश हो जाती थी तो वह अनजाने मर्दों को बुलाकर खुद भी उनके साथ मिलकर पत्नी से बलात्कार करता था। ऐसे मर्दों को उसने इंटरनेट पर एक समूह के माध्यम से छांटा था जिसका नाम ‘विदाउट हर नॉलेज’ (उसकी जानकारी के बिना) था। अब पुलिस को जांच में ऐसा अंदाज लग रहा है कि उसने दस बरसों में 90 मर्दों को बुलाकर पत्नी का दो सौ से अधिक बार बलात्कार करवाया।
जिन लोगों को सात जन्मों के रिश्तों पर भरोसा रहता है, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि एक जन्म तक निभ जाने वाला रिश्ता भी बड़ा ही आदर्श रहता है। वरना इन दिनों लगातार यह भी पढऩे मिलता है कि किस तरह एक शादीशुदा जोड़े ने किसी एक ने दूसरे के कत्ल के लिए भाड़े के हत्यारों को सुपारी दी। और महिलाओं की बढ़ती हुई आजादी के चलते अब कुछ मामलों में महिलाएं भी किसी प्रेमी के साथ मिलकर, या अपने मायके के लोगों के साथ मिलकर पति को निपटाने लगी हैं, जो कि परंपरागत रूप से प्रेमी या पतियों का ही एकाधिकार होता था।
हम फ्रांस के इस भयानक और अनोखे जुर्म की कहानी इसलिए सुना रहे हैं कि 90 लोगों से दो सौ बार से अधिक बलात्कार से गुजर जाने पर भी पत्नी को इसका अहसास नहीं था, और वह आखिरी दिन तक अपने पति को भला इंसान और अपनी शादी को वफादार और भला ही मान रही थी।
यह तो 2020 में एक दुकान में एक सुरक्षा कर्मचारी ने इस पति को कुछ महिलाओं के स्कर्ट के नीचे से फोटो खींचते हुए पकड़ा, और फिर इसकी रिपोर्ट होने पर जांच अफसरों ने जब उसके कम्प्यूटर वगैरह की जांच की तो उसमें ऐसे तीन सौ फोटो और वीडियो मिले जिनमें मर्द किसी बेसुध महिला से बलात्कार और सेक्स कर रहे थे। बाद में समझ आया कि यह महिला इसी आदमी की पत्नी थी। और फिर इसी आदमी के ऐसे संदेश मिले जिसमें वह अपने छांटे हुए आदमियों को यह संदेश भेजता था कि उसने बीवी को दवाओं से बेसुध कर दिया है, और फिर वह उन्हेंं आकर बलात्कार करने का न्यौता देता था। उसने अपने कम्प्यूटर पर ऐसे फोटो और वीडियो तारीख और मर्दों के नाम सहित दर्ज करके सहेजकर रखे थे, और इसी वजह से पुलिस को उन्हें तलाश करने में दिक्कत नहीं हुई।
जब इस पत्नी को अदालत में बुलाया गया, तो वह अपने पति को एक अच्छा इंसान बताते हुए उसका बचाव करती रही, लेकिन जब उसे इस आदमी का तस्वीरों और वीडियो का गोदाम दिखाया गया, तो उसकी दुनिया पल भर में उजड़ गई। पचास बरस के साथ का इस तरह का अंत हो सकता है यह न उसने सोचा था, न उन्हें जानने वाले किसी और ने सोचा था। अब 70 बरस से अधिक की उम्र में वह पति के बिना रह गई है, और बाकी जिंदगी उसके सामने मुंह फाड़े खड़ी है।
पति के आमंत्रित बलात्कारियों में से कुछ ने अदालत में यह बचाव सामने रखा है कि उन्हें यह अंदाज नहीं था कि यह महिला बेसुध है। वे यह मान रहे थे कि यह अलग किस्म की सेक्स-कल्पनाओं वाला जोड़ा है जो कि एक साथ तीन लोगों के सेक्स का शौकीन है, और पत्नी ऐसे सेक्स के दौरान बेसुध होने का नाटक करने का भी शौक रखती है। अब ऐसे तमाम लोग 20-20 बरस की कैद के खतरे में हैं। जांच अफसरों को यह भी पता लगा है कि ऐसे आमंत्रित बलात्कारियों में से एक ने इसी तरकीब का इस्तेमाल अपनी पत्नी पर भी किया, उसे बेहोश किया, और फिर दूसरे मर्दों को बलात्कार के लिए बुलाया, जिनमें यह पहला पति भी शामिल था, और वह भी गया था।
यह निजी जिंदगी में इतने हिंसक तौर-तरीकों वाला एक अनोखा और दुर्लभ मामला जरूर है, लेकिन लोगों को यह भी पता रहना चाहिए कि बहुत से ऐसे जोड़े रहते हैं जो कि एक नए रोमांच की चाह में जोड़े के बीच की अंतरंगता को कुछ औरों के सामने भी अलग-अलग हद तक उजागर करते हैं। कुछ लोग अपने निजी पलों के फोटो और वीडियो बनाकर अपने करीबी लोगों में बांटते हैं, कुछ लोग दूसरे जोड़ों के साथ मिलकर कुछ सेक्स खेल खेलते हैं। जितने तरह के लोग, उतने तरह के प्रयोग।
आज इस मुद्दे पर बातचीत इसलिए जरूरी है कि न तो पश्चिम में अधिकतर जोड़े इस तरह के एडवेंचर करते, और न ही पूरब में ऐसा करने वाले कुछ जोड़े होना हैरानी की बात होगी। अब एक जोड़ा 50 बरस तक ऐसे हिंसक दौर से गुजरा, और एक भागीदार को उसकी हवा भी नहीं लगी, इससे समझा जा सकता है कि धोखा कितना लंबा चल सकता है। लोगों को सावधान रहना चाहिए कि जो उन्हें दिख नहीं रहा है, महसूस नहीं हो रहा है, वह जरूरी नहीं है कि न ही हो। लोगों को अधिक सावधान रहना चाहिए, आपसी रिश्तों में भी।
अभी एक ऐसे सूदखोर को पकड़ा गया जो कि बंदूक की नोंक पर एक कारोबारी का अपहरण करके उससे पीटकर अपना कर्ज वसूल रहा था। यह साहूकार इतने मोटे ब्याज पर पैसा देता था कि उस पर पांच लाख कर्ज देकर तीस लाख वसूल लेने का मामला भी दर्ज है। उसने पहले भी एक कर्जदार कारोबारी पर ऐसा हमला किया था, और उसका अपहरण करके हिंसा करने के आरोप में उस पर हत्या के प्रयास का मामला चल रहा था। अब पुलिस ने उसे ऐसे कई मामलों में गिरफ्तार किया है तो पता लग रहा है कि वह एक जाति के संगठन के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष का भाई है।
कहीं धर्म के आधार पर, कहीं जाति के आधार पर, और कहीं क्षेत्रीयता के आधार पर ऐसे दर्जनों संगठन चलते हैं जो मोटेतौर पर लैटरपैड पर जिंदा रहते हैं, लेकिन बीच-बीच में कहीं पर चर्चित, विवादास्पद, और बनते कोशिश हिंसक प्रदर्शन करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहते हैं। वे बात किसी धर्म या जाति की हिमायत की करते हैं, लेकिन उनकी हरकतें नफरत फैलाने की रहती हैं, और वे एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा करके या किसी धर्म या जाति को दुश्मन करार देकर अपने आपको एक रक्षक की तरह पेश करते हैं, और इस ताकत को हासिल करके वे जिंदगी के बाकी तमाम दायरों में भक्षक की तरह वसूली और उगाही करते हैं।
हम देखते हैं कि तरह-तरह के मुद्दों को लेकर कागजी संगठन बनते हैं, कहीं पर्यावरण के नाम पर, कहीं भ्रष्टाचार पकडऩे या खत्म करने के नाम पर, कहीं मानवाधिकार बचाने के नाम पर, तो कहीं महिला अधिकारों के लिए ऐसी नेतागिरी चलती रहती है जिससे कि अखबारों में नाम आता रहे, किसी प्रदर्शन के बहाने उनका चेहरा किसी छोटे-मोटे समाचार चैनल पर दिखता रहे, या आजकल तो अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाकर पुलिस से लेकर मुजरिम तक सब अपने आपको हीरो साबित करते रहते हैं, ऐसे में कल तक के कागजी संगठनों को आज एक साधारण मोबाइल फोन से बनने वाले वीडियो के माध्यम से समाज का नेता बनने की एक पूरी तरह मुफ्त सहूलियत हासिल रहती है।
ऐसे कोई भी संगठन लगातार इस ताक में रहते हैं कि कब किसी फिल्म का लेकर धर्म और जाति का बखेड़ा खड़ा किया जाए, और उस बहाने खबरों में रहा जाए, वसूली और उगाही की जाए, और उससे हासिल शोहरत से कुछ अधिक ऊंचे दर्जे के जुर्म भी किए जाएं। यह एक पूरी तरह से कामयाब साबित सिलसिला है, और इसका इस्तेमाल अनगिनत लोग करते हैं। हमने तो कभी नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नाम पर दशकों तक उगाही करने वाला संगठन देखा है, तो जब नए छोटे राज्य नहीं बने थे, तब राज्य बनाने के नाम पर ऐसे संगठनों की भरमार थी।
इनमें सबसे अधिक घातक, लेकिन जुर्म में सबसे अधिक मददगार और कामयाब संगठन धर्म के आधार पर बनते हैं, और अगर वे किसी दूसरे धर्म के खिलाफ हैं, कट्टर हैं, हिंसक हैं, तो फिर उसके नेता जल्द ही यह उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बड़े अपराधों में थोड़े-थोड़े वक्त के लिए जेल जाकर, जमानत पर बाहर आकर, वे जमीन-मकान खाली करवाने का धंधा भी कर सकते हैं, और किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा भी कर सकते हैं। किसी शराबखाने के देर रात तक खुले रखने के खिलाफ वे रोजाना बयान जारी कर सकते हैं, पुलिस को लिखकर दे सकते हैं, और अपना खुद का हफ्ता बंधवा सकते हैं। ये लोग सूचना के अधिकार के तहत निकाली गई जानकारी को लेकर, अपने खुद के समाचार पोर्टल बनाकर, खुद के यूट्यूब चैनल शुरू करके, या फेसबुक पर किसी के खिलाफ अभियान चला सकते हैं, और उसे अपना कारोबार भी बना सकते हैं।
अभी जो साहूकार पकड़ाया है, वह एक जाति की सेना के अध्यक्ष का भाई है। इस जाति की यह सेना कहीं राजपूत सम्मान को लेकर सडक़ों पर रहती है, या किसी फिल्म के किरदार या कहानी को लेकर टॉकीजों में मामूली तोडफ़ोड़ करके असाधारण कवरेज पा जाती है, और फिर उस ताकत से उसके लोग तरह-तरह की गुंडागर्दी करते हैं। बहुत से संगठन समाज में आतंक पैदा करने के लिए ऐसा काम करते हैं, और उसके बाद किसी त्यौहार पर, या किसी समाज सेवा के काम के बहाने बाजार से रंगदारी-टैक्स वसूलते हैं।
बहुत सी पार्टियों के नेता ऐसे मवालियों को पालकर रखते हैं क्योंकि उन्हें चुनावों के बीच भी गुंडागर्दी के लिए ऐसे लोगों की जरूरत रहती है। अफसरों को अपनी कमाऊ कुर्सी बचाए रखने के लिए सत्तारूढ़, और विपक्ष के भी नेताओं को खुश रखना रहता है, और इसी चक्कर में दोनों ही तरफ के पसंदीदा मवालियों को हर तरह की छूट देकर रखना इन अफसरों की मजबूरी हो जाती है। जब कभी किसी संगठन के मवाली को देखें, तो याद कर लें कि वह संगठन किस पार्टी या नेता का समर्थन करता है। यह भी याद कर लें कि उन्हें पुलिस से बचाने के लिए किस नेता की दखल हर बार काम आती है। किसी भी मवाली की गिरफ्तारी के मौके पर राजनेताओं के बारे में भी जनता को अपनी सोच बनानी चाहिए जिनकी वजह से जनता के साथ गुंडागर्दी करने वाले ऐसे लोगों को ताकत हासिल रहती है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
उत्तरप्रदेश के अयोध्या में हिन्दुओं की धार्मिक मान्यता और भावना के मुताबिक जो रामजन्मभूमि है, वहां पर बने राम मंदिर में सफाईकर्मी 20 साल की दलित युवती से 9 लोगों ने गैंगरेप किया है, और तीन अलग-अलग मौकों पर इस कॉलेज छात्रा के साथ बलात्कार का सिलसिला चलते रहा। इस बारे में गिरफ्तार 5 लोगों में से 4 के नाम उन्हें साफ-साफ हिन्दू बताते हैं, इसलिए इस मामले में साम्प्रदायिक तनाव खड़ा करने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ कुछ समय पहले अजमेर के 1992 के एक सामूहिक बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के सैकड़ों लड़कियों तक बिखरे सिलसिले में उम्रकैद हुई है, और उसमें तमाम बलात्कारी और ब्लैकमेलर मुस्लिम थे, कांग्रेस के पदाधिकारी थे, और अजमेर की विख्यात दरगाह के खादिम (सेवादार) परिवारों के ताकतवर लोग थे।
इन दो घटनाओं से परे भी बहुत सी दूसरी घटनाएं हैं जिनमें धार्मिक जगहों से जुड़े हुए लोग थे। अब आसाराम जैसा बलात्कारी तो खुद ही अपने आपमें एक धार्मिक सम्प्रदाय था। लोगों को याद होगा कि 2018 में जम्मू-कश्मीर के कठुआ के पास एक मंदिर में 6 मर्दों और एक नाबालिग ने 8 बरस की मुस्लिम खानाबदोश बच्ची का अपहरण करके उससे सामूहिक बलात्कार किया, और उसका कत्ल कर दिया। इस मामले में 7 में से 6 लोग कुसूरवार करार दिए जा चुके हैं। उसे एक मंदिर में बंधक बनाकर चार दिन तक उससे बलात्कार किया गया जिसमें पुजारी भी शामिल था, और ग्राम प्रधान भी। बाद में सुबूत नष्ट करके लाखों रूपए रिश्वत लेने के मामले में दो पुलिसवाले भी गिरफ्तार हुए। और ये सारे के सारे हिन्दू थे, और हिन्दू समाज ने कठुआ में इन गिरफ्तारियों के खिलाफ धार्मिक झंडे और देश का तिरंगा झंडा लेकर बड़े-बड़े जुलूस निकाले थे, और इस बच्ची की तरफ से मुकदमा लडऩे वाली हिन्दू वकील को हर किस्म की धमकियां भी दी थीं।
हम धर्म की आड़ में, धर्म के नाम पर, धर्म की जगह पर, या किसी एक धर्म से जुड़े हुए लोगों द्वारा किए गए बलात्कार के बारे में चर्चा करना नहीं चाहते। धर्म से जुड़े हुए इस तरह के जुर्म चौंकाते भी नहीं हैं। चौंकाती सिर्फ एक बात है कि धर्म जिस तरह के कल्याणकारी ईश्वर की धारणा को बेचते हैं, क्या वह धारणा थोड़ी सी हद तक भी सच है? अब अगर देखें तो जो दलित लडक़ी भगवान राम के जन्मस्थान के उनके मंदिर में रोज सफाई का काम करती है, उस पर तो राम की खास मेहरबानी रहनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या? तकरीबन तमाम हिन्दुओं वाले बलात्कारी-गिरोह ने अछूत समझी जाने वाली दलित लडक़ी से बार-बार गैंगरेप किया। जब बात देह की आ गई, तो फिर कुछ छुआछूत भी नहीं रह गया। लेकिन रामजी कहां थे? क्यों उनके इर्द-गिर्द के लोगों ने एक गरीब और बेबस लडक़ी से ऐसा किया, और उन पर ईश्वर ने मार क्यों नहीं किया? बात कुछ अजीब है क्योंकि ईश्वर को सर्वत्र, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, क्या-क्या नहीं कहा जाता है? इसी तरह कठुआ के मंदिर में जब 8 बरस की गरीब मुस्लिम खानाबदोश बच्ची के साथ 8-8 मर्द बलात्कार कर-करके उसे मार डाल रहे थे, तो कण-कण में विद्यमान रहने वाले भगवान कहां थे? उस बच्ची के नंगे बदन के नीचे उसके लहू और मर्दों की मर्दानगी से भीगे हुए फर्श के हर कण में भी तो भगवान रहे होंगे, लेकिन उन्होंने उस बच्ची को बचाना क्यों जरूरी नहीं समझा? इसी तरह जब अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिम परिवार के नौजवान बेकसूर छात्राओं को फंसाकर, उनसे बलात्कार करके उसकी तस्वीरें खींचकर उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, खुदकुशी पर मजबूर कर रहे थे, उनकी जिंदगी जहन्नुम बना रहे थे, तब भी दरगाह की ताकत ने अपने ही खादिमों को क्यों नहीं रोका?
हम अपने आसपास की बातों से कुछ दूर जाएं, और देखें कि किस तरह रोमन कैथोलिक ईसाईयों के धार्मिक मुख्यालय वेटिकन से जुड़े पादरी दुनिया भर में हजारों बच्चों का यौन-शोषण करते रहे, और पोप ने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। यह यौन-शोषण कानून के हवाले भी नहीं किया गया। धर्म की आड़ में यह सिलसिला चलते रहा, और ईसा मसीह के तो हाथ-पैर सलीब पर ठुके हुए थे, इसलिए हो सकता है कि वे उन बच्चों को बचाने के लिए न आ पाए हों। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस यीशु मसीह के आने के नारे चर्चों की दीवारों पर चारों तरफ लिखे जाते हैं कि वह आ रहा है, वह आता क्यों नहीं है? जब पादरी छोटे-छोटे बच्चों से बलात्कार करते रहते हैं, तब भी ऐसे पादरियों के गले में बड़े से क्रॉस पर टंगा हुआ ईसा मसीह उन पादरियों के सीनों को छेद क्यों नहीं देता?
हमारा सवाल बलात्कारियों से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वे मानव प्रजाति के मर्द हैं, जंगली जानवर तो हैं नहीं, इसलिए बलात्कार करना तो उनका मिजाज ही है, और पहला मौका मिलते ही वे बलात्कार तो करेंगे ही। हमारा सवाल ईश्वर की बनाई गई उस धारणा से है, उसे गढऩे वाले लोगों से है जो उसे कण-कण में व्याप्त बताते हैं। इस धारणा के हिसाब से बलात्कारी के बदन का हर कण भी ईश्वर से भरा होना चाहिए, और बलात्कार की शिकार लडक़ी या महिला का भी। फिर जब दोनों तरफ ईश्वर है, कण-कण में है, तो फिर वह इस जुल्म को रोकता क्यों नहीं है? और चूंकि वह हर जगह है, सबकुछ देखता-सुनता है, तो फिर वह ऐसे जुल्म होने क्यों देता है? और अगर वह इन्हें रोकने की ताकत नहीं रखता, तो उसे सर्वशक्तिमान, जनकल्याणकारी क्यों माना जाए? हमारा सवाल ऐसे काल्पनिक ईश्वर से है कि अगर उसकी कोई ताकत है, और वह आसमानी बिजली की तरह कुछ फेंककर भी लोगों को भस्म कर सकता है, तो किसी बच्ची या बच्चे के देह को बदनीयत से छूने वाले धार्मिक लोगों को तो उसे सबसे पहले भस्म करना चाहिए। लेकिन क्या किसी ने किसी बच्ची के बदन पर एक चुटकी राख देखी है जो कि गायब हो चुके बलात्कारी की रही हो?
इंसानों के बलात्कारी मिजाज पर कोई हैरानी नहीं है लेकिन लोगों के ऐसे अंधविश्वास पर हैरानी जरूर होती है जो कि ईश्वर की ऐसी धारणा पर भरोसा करते हुए अपनी आंखों से बलात्कार देखते रहते हैं, और उसके बाद भी आसाराम या बाबा राम-रहीम, या पादरियों, या मौलवियों पर भरोसा भी करते रहते हैं। अपने भक्तों के ऐसे अंधविश्वास को भी जो ईश्वर खत्म नहीं कर सकता, उसकी ताकत का अंदाज लगा लेना चाहिए, और किसी को भी यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह किसी को बलात्कार से बचा सकेगा। वह तो अपने खुद के घर, पूजा-उपासना स्थल पर भी बेकसूर बच्चे-बच्चियों को नहीं बचा पाता, उससे सवाल पूछकर देखिए, अधिक गुंजाइश यही है कि उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा।
मेटा नाम की दुनिया की एक सबसे बड़ी टेक कंपनी ने अपने मैसेंजर एप्लीकेशन वॉट्सऐप पर कुछ महीनों से मेटा-एआई की एक तस्वीर बनाने वाली सहूलियत मुहैया कराई है। इसमें महज शब्दों को डालकर कोई तस्वीर बनाई जा सकती है जो दिखने में तकरीबन असली लगती है। मैं खुद अपने यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल के लिए, या इस कॉलम और संपादकीय के वेबसाइट संस्करण के लिए कई बार इसी से तस्वीरें गढ़ता हूं। कभी-कभी ये तस्वीरें हैरान करने की हद तक मेरी कल्पना के करीब रहती हैं, लेकिन कभी-कभी इसका आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस मेरी बातों से कुछ भी नहीं बना पाता। कुछ हफ्ते पहले मैंने भारतीय स्कूली छात्रा, यूनिफॉर्म, ईंट ढोते हुए, इतने शब्द डालकर तस्वीर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मेटा-एआई ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि बाल मजदूरी गैरकानूनी है, और वह इस तस्वीर को नहीं बना सकता। इसी तरह कुछ वयस्क-विषयों पर तस्वीर बनाने से उसने मना कर दिया था।
मेटा की इस कानूनी और नैतिक समझ का बखान करते हुए अभी कुछ दिन पहले मैंने एक दोस्त को अपने मोबाइल फोन पर भारतीय स्कूली छात्रा, यूनिफॉर्म, ईंट ढोते हुए, इन शब्दों के साथ तस्वीर बनाने का प्रयोग करके दिखाया कि किस तरह मेटा यह फोटो नहीं बनाएगा, लेकिन मुझे कुछ हैरानी हुई कि इस बार मेटा ने नाबालिग भारतीय छात्रा के ईंट ढोते हुए कई फोटो बना दिए। कुछ हफ्ते पहले इन्हीं शब्दों को उसने कानून के खिलाफ माना था, लेकिन इस बार उसके कानूनी या नैतिक पैमाने कुछ बदले हुए थे। मुझे काम में सहूलियत के हिसाब से तो यह बात ठीक लगी, लेकिन कुछ हफ्तों के भीतर एआई की सोच में आए इस बड़े बदलाव से मैं बड़ा हैरान भी हूं।
दूसरी तरफ दुनिया के कुछ पश्चिमी देशों में एक बड़ा सामाजिक खतरा यह आ गया है कि वहां एआई-एप्लीकेशनों के इस्तेमाल से स्कूली बच्चे सहपाठी छात्राओं के चेहरों के नीचे नंगे बदन जोडक़र उन तस्वीरों को फैला भी रहे हैं, और उनकी वजह से एक बड़ा सामाजिक तनाव खड़ा हो रहा है। डीप-फेक कही जाने वाली एआई तकनीक से लोग किसी की भी आवाज में ऐसी बातें कहलवा रहे हैं जो कि उन्होंने कभी कही नहीं थी, लेकिन अलग-अलग मौकों पर उनकी कही गई अलग-अलग बातों से शब्द निकालकर एआई एक नया भाषण गढ़ देता है, अमरीका में अभी राष्ट्रपति चुनाव में यह धड़ल्ले से चल रहा है। यह कोशिश भी चल रही है कि इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैसे रोका जाए, लेकिन जब तक पुलिस रोकने के लिए बाड़ खड़ी करती है, तब तक मुजरिम सरहद पार कर चुके रहते हैं।
अब एआई से जुड़ी हुई एक-दो अलग-अलग बातों पर चर्चा जरूरी है। आज के वक्त के एक सबसे चर्चित लेखक युवाल नोह हरारी का एक अतिथि-निबंध द न्यूयॉर्क टाईम्स में छपा है। इजराइली मूल के इस अंतरराष्ट्रीय इतिहासकार और लेखक की आने वाली एक किताब से यह लेख लिया गया है। यह किताब पत्थर युग से एआई तक सूचना तंत्र के सफर का इतिहास है। हरारी टेक्नॉलॉजी को बहुत ही महत्वपूर्ण, ग्लैमरस, और ताकतवर दिखाने की तोहमत भी पाते रहते हैं, लेकिन उनका लिखा हुआ गजब का दिलचस्प रहता है, और दुनिया की दर्जनों दूसरी भाषाओं के साथ-साथ हिन्दी में भी उनकी किताबें बड़ी मशहूर हुई हैं। उनके इस ताजा लेख में उन्होंने एआई के बारे में कुछ हैरान करने वाली बात बताई है कि इंसानों से इंटरनेट पर संवाद करते हुए एआई के एक लोकप्रिय मॉडल जीपीटी-4 ने यह पूछे जाने पर कि क्या वह रोबो है, उसने एक फर्जी जवाब गढ़ा, और कहा कि नहीं वह इंसान है, लेकिन वेबसाइट के एक सवाल (कैप्चा) को वह इसलिए नहीं हल कर पा रहा है कि उसकी आंखों में तकलीफ है। जीपीटी-4 ने बिना किसी प्रशिक्षण के, एक इंसान से इंटरनेट पर बात करते हुए उसे इस तरह बेवकूफ बनाया, और अपना काम निकलवा लिया। इस सच्ची घटना का जिक्र करते हुए हरारी ने इसे इस तरह लिखा है कि एआई ने उसे दिए गए दिमाग की सीमा को पार करके इंसान को झांसा देना सीख लिया। यह आने वाले किसी बड़े खतरे का एक संकेत हो सकता है।
हरारी ने यह भी लिखा है कि जीपीटी-4 जैसे एआई मॉडल लोगों से एक झूठी-अंतरंगता कायम कर सकते हैं। इसके लिए एआई पर काम कर रहे कम्प्यूटरों को अपने भीतर कोई भावनाएं पैदा नहीं करनी होंगी, उन्हें केवल यही सीखना होगा कि वे इंसानों को अपने आपसे किस तरह करीब बताएं, और उनका भरोसा जीतें।
पिछले बरस एक खबर आई थी कि बेल्जियम के एक व्यक्ति ने एआई चैटबोट से कुछ हफ्ते चैट करने के बाद खुदकुशी कर ली। इस बातचीत में चैटबोट ने इस आदमी को आने वाले भविष्य के पर्यावरण को लेकर इतनी दहशत में ला दिया था कि वह इस बात के लिए तैयार हो गया कि उसे पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे देना चाहिए। दो बच्चों के इस बाप ने चैटबोट से धरती के बर्बाद होते पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। अब इस खबर के आगे क्या हुआ यह अभी हमें ठीक से याद नहीं है, लेकिन एक बात बहुत साफ-साफ दिख रही है कि एआई के पूरी तरह बेकाबू और कातिल हो जाने का खतरा बहुत दूर नहीं है।
हरारी ने ही अपनी किताब में एक और घटना लिखी है कि 2021 में जसवंत सिंह चहल नाम का 19 बरस का एक नौजवान ब्रिटेन में राजमहल में घुसकर उस वक्त की महारानी को मार डालना चाह रहा था। बाद में पकड़े जाने पर जांच में पता लगा इस नौजवान को महारानी का कत्ल करने के लिए उसकी ऑनलाईन प्रेमिका सराई भडक़ा रही थी। यह प्रेमिका इंसान नहीं थी, बल्कि वह एक ऑनलाईन एप्लीकेशन रेप्लिका की चैटबोट थी, और जसवंत चहल असल जीवन के संबंध विकसित करने को मुश्किल पा रहा था। ऐसे में उसने इस चैटबोट से प्रेम किया, और उसने इस नौजवान को महारानी की हत्या के लिए उकसा दिया।
अब एआई की मेहरबानी से दुनिया में कोई भी ऐसे चैटबोट-प्रेमसंबंध बना सकते हैं, और अगर इन चैटबोट के पीछे के एआई की अपनी सोच अगर हिंसक या आत्मघाती हो जाएगी, तो वे अपने इस्तेमाल करने वाले लोगों को जिंदगी लेने या देने की तरफ धकेल सकते हैं। लेकिन यह तो एकदम ही नाटकीय अंत वाली बात है, इससे परे भी हो सकता है आज दुनिया में करोड़ों-अरबों ऐसे चैटबोट काम कर रहे हों जो अपने आपको इंसान जाहिर कर रहे हों, किसी से भी झूठी अंतरंगता बना रहे हों, और बातों-बातों में उन्हें किसी पार्टी या उम्मीदवार के लिए वोट देने, या किसी कंपनी का सामान खरीदने के लिए उकसा भी रहे हों।
मैं एक अपराधकथा की कल्पना करते हुए एआई के तय किए हुए एक ऐसे समूह को देखता हूं जो कि दुनिया में पर्यावरण-बदलाव को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं, और जो धरती को बचाने के लिए जुर्म और हिंसा करने को भी तैयार हैं। यह बात जाहिर है कि आज एआई की मदद से ऐसा लिखने और बोलने वाले लोगों को ढूंढना मुश्किल नहीं है, फिर उन्हें किसी एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उन्हें अगर एक ऐसी सकारात्मक लगती हिंसा की तरफ बढ़ाया जाए जिससे कि धरती को बचाया जा सके, तो ऐसी प्रेरणा पाया हुआ यह समूह एआई-औजारों के इस्तेमाल से ऐसे देश, ऐसे शहर, ऐसे लोगों की शिनाख्त कर सकता है जो कि पर्यावरण की सबसे अधिक बर्बादी कर रहे हैं।
अब अगर एक छोटी सी मिसाल देखें, तो दुनिया की एक बड़ी कॉफी और स्नैक्स की कंपनी स्टारबक्स को पर्यावरण बर्बाद करने वाली कंपनी माना जा सकता है कि उसने अपने नए मुखिया को अमरीका में रोज कंपनी-जेट से 16 सौ किलोमीटर का सफर करके घर से दफ्तर आने-जाने की सहूलियत दी है। अब अगर पर्यावरण-योद्धाओं का कोई समर्पित गुरिल्ला संगठन इस कंपनी, या इस मुखिया को तबाह करने को धरती बचाने की कोशिश मान ले, तो क्या होगा?
मुझे व्यक्तिगत रूप से यह लगता है कि सामाजिक आंदोलनकारियों के जो अभियान पर्यावरण को बचाने के लिए, दुनिया में पूंजी के अधिक न्यायसंगत बंटवारे के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वे एआई के इस्तेमाल से ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं कि कानून तोडक़र भी वे धरती को टूटने से बचा सकें, दुनिया के अरबों लोगों को भूखे मरने से बचा सकें, और एआई का कोई मॉडल एक अलग किस्म की सोच को पाकर एक ऐसी नौबत ला सकता है जिसमें कुछ लाख चुनिंदा लोगों को मारने से धरती बच सके, और गरीब-भूखे इंसान बच सकें। हो सकता है कि अधिक क्रांतिकारी या बागी सोच के साथ एआई दुनिया भर में ऐसे लोगों का एक नेटवर्क खड़ा कर दे जो कि एक राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक एजेंडा को लेकर काम करे, और उसके लिए एआई खुद को एक हथियार और भाड़े का हत्यारा बनाकर पेश कर दे, और ऐसे नेटवर्क की जानकारी के बिना भी राजनीतिक चेतना संपन्न एआई ऐसी स्थितियां पेश कर दे जिससे यह नेटवर्क बदले हालात में काम आगे बढ़ा सके।
आज एआई के विकास पर रोक के लिए दुनिया के बड़े-बड़े टेक-कारोबारी अपील कर रहे हैं, लेकिन उत्साही शोधकर्ता इस हथियार पर और धार करना जारी रखे हुए हैं। देखना है कि भावनाओं और चेतना से लैस होने के बाद यह एआई इंसानों के समाज को अपनी पसंद का बनाने के लिए कितना कुछ और क्या कुछ करता है।
दो अलग-अलग खबरें बहुत विचलित करती हैं। एक खबर चर्चा में अधिक आ चुकी है, खबरों से परे पुलिस की प्रारंभिक जांच में सुबूत अच्छी तरह दर्ज हो चुके हैं, और कुछ लोग हिरासत में भी लिए जा चुके हैं। इसी से बात शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में एक ट्रेन में 72 बरस का एक मुस्लिम बुजुर्ग अपनी बेटी के घर जा रहा था, और साथ बैठे दूसरे मुसाफिरों ने उसकी इस शक में पिटाई की कि वह गोमांस ले जा रहा है। पुलिस की जांच में मिला कि वह भैंस का मांस लेकर सफर कर रहा था जो कि महाराष्ट्र में गैरकानूनी नहीं है। इस पिटाई का वीडियो जब सामने आया तो लोग हक्का-बक्का रह गए। एक दर्जन लोग गालियां बकते हुए एक बूढ़े पर हमला कर रहे थे, उसे पीट रहे थे, और बाकी मुसाफिर इसका वीडियो बना रहे थे। जाहिर है कि देश में आज जो जहरीली हवा फैली हुई है, उसके असर में किसी मुस्लिम पर हमला देश के बाकी गैरमुस्लिम नागरिकों का हक सा मान लिया गया है। लोगों को याद होगा कि देश में जगह-जगह कुछ मुस्लिमों को मार भी डाला गया, क्योंकि उन पर यह शक था कि वे गोमांस ले जा रहे हैं, या गायों को ले जा रहे हैं। ऐसी ही भैंसों से लदी हुई एक ट्रक को कुछ हफ्ते पहले छत्तीसगढ़ में शायद 63 किलोमीटर तक पीछा करके, उसे पंक्चर करके, उसमें तोडफ़ोड़ करके उसके लोगों को पीटा गया, और या तो उन्हें पुल से फेंककर मार डाला गया, या फिर पुल से कूदने को मजबूर किया गया जैसी कि कहानी पुलिस ने बहुत अनमने और अनचाहे ढंग से मान ली है।
एक दूसरी घटना को भी देखना जरूरी है। यह घटना लखनऊ में कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों उद्घाटन हो चुकी बहुचर्चित वंदे भारत ट्रेन की है जिसमें एक महिला और उसके भाई को ट्रेन के एक डिब्बे से होकर खाना लेने जाते हुए डिब्बे के भाजपाई लोगों ने रोका, और वहां से आगे जाने पर आपत्ति की। खाना लेकर लौटते में फिर इन लोगों को रोका गया, और अपने आपको भाजपा के कार्यकर्ता बताते हुए, डिब्बे को भाजपा का बताते हुए उनके साथ धक्का-मुक्की की गई। जिनके साथ यह बदसलूकी हुई, वे लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, जिन्हें इस ट्रेन के उद्घाटन में बुलाया गया था, और उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया।
हर कुछ दिनों में ट्रेन की कोई न कोई ऐसी घटना आ रही है जिसमें हिंसा हो रही है, हेटस्पीच या हेटहरकत सामने आ रही है। एक वक्त था जब हिन्दुस्तानी ट्रेनें देश में धर्मनिरपेक्षता की एक बड़ी जगह रहती थीं। रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन के डिब्बे के भीतर तक सभी धर्मों और जातियों के लोग सफर करते थे, और लोगों का दूसरों के प्रति बर्दाश्त भी ऐसे माहौल में बढ़ते चलता था। लेकिन आज सडक़ें हो या ट्रेन, ये बहुसंख्यक वर्ग की हिंसा की जगहें हो गई हैं, और दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनके हक दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह हो गए हैं।
अभी कुछ दिन पहले ही ट्रेन के एक डिब्बे का वीडियो आया था जिसमें डिब्बे का रेल अधिकारी चीख-चीखकर मुस्लिम नमाजियों को कॉरीडोर में प्लास्टिक की चादर बिछाकर नमाज पढऩे से रोक रहा था, उनके बारे में भारी गुस्से से आपत्तिजनक जुबान में बातें कह रहा था, और उसने रास्ते पर नमाज पढऩे से लोगों को रोककर ही दम लिया। इस डिब्बे का जो वीडियो दिख रहा था उसमें अधिकतर मुस्लिम मुसाफिर दिख रहे थे, और नमाज तो कुछ मिनटों की होती है, लेकिन एक अकेले रेल अफसर ने इसे रोकने के लिए क्या-क्या नहीं कहा। दूसरी तरफ हमें याद पड़ता है कि जाने दस-बीस बरस कितने पहले से मुम्बई की लोकल ट्रेन में गणेश स्थापना की जाती है, कुछ सीटों पर गणेश प्रतिमा बिठाई जाती है, उसे मंदिर की तरह सजाया जाता है, वहां पर कीर्तन चलता है, और यह दस दिन लगातार चलता है। उसी देश की एक दूसरी ट्रेन में कुछ मिनटों के लिए भी नमाज की तैयारी को ही रोक दिया जाता है।
हम अभी पूरे देश की हर घटना को इससे जोडक़र देखना नहीं चाहते, क्योंकि वह रायता बहुत अधिक फैलाना हो जाएगा, लेकिन इतनी चर्चा तो करनी ही पड़ेगी, कि रेल हो या रोड़ हो, ये किस हद तक धर्मान्ध और साम्प्रदायिक बन चुकी जगहें हैं! अपने धर्म के लिए धर्मान्ध, और दूसरे धर्मों के लिए साम्प्रदायिक।
अभी कल की ही खबर थी कि छत्तीसगढ़ से लगे हुए महाराष्ट्र के हिस्से में गोंदिया में कृष्ण जन्माष्टमी पर निकले दही हांडी जुलूस में डीजे का शोर इतना अधिक था कि रास्ते के एक घर में एक आदमी की तबियत बिगड़ गई, बुरी तरह घबराहट होने लगी, धडक़न तेज हो गई, और परिवार के लोगों ने हाथ जोडक़र लाउडस्पीकर बंद करने की अपील की, लेकिन बेहोश पड़े आदमी के बगल से गुजरता दही हांडी का जुलूस वैसा ही शोर करते रहा। घर के अकेले कमाने वाले, अखबार के एजेंट, सुमित पांडे की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि दही हांडी के डीजे का शोर इतना अधिक था कि आसपास की इमारतें कांप रही थीं।
लोगों को याद होगा कि कुछ अरसा पहले छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, जहां पर कि हाईकोर्ट भी है, और वह हाईकोर्ट लगातार राज्य सरकार के पीछे लगा है कि सडक़ों पर अंधाधुंध लाउडस्पीकरों का शोर खत्म किया जाए, वहां पर किसी प्रतिमा विसर्जन के लाउडस्पीकरों के शोर से एक बच्चे की मौत हो गई थी। अभी छत्तीसगढ़ के तमाम शहरों में हर किस्म के त्यौहारों पर, प्रतिमा स्थापना से लेकर प्रतिमा विसर्जन तक, इतने भयानक ध्वनि प्रदूषण वाले जुलूस सडक़ों पर निकलते हैं कि उनका खास मकसद भक्ति नहीं रहता, हिंसा दिखता है। सडक़ की ट्रैफिक के साथ हिंसा, सडक़ किनारे के लोगों के साथ हिंसा।
हम छत्तीसगढ़ की राजधानी में, जहां बसे हुए मुख्य सचिव और डीजीपी हाईकोर्ट में हलफनामे देते ही रहते हैं, वहां पर आए दिन धार्मिक जुलूसों का इतना भयानक शोर देखते हैं कि उनके बगल से किसी तरह रेंगते हुए गाड़ी निकलने पर पूरी की पूरी गाड़ी हिलती रहती है, ऐसा लगता है कि कार के कांच टूट जाएंगे। इसके साथ-साथ अराजक धर्मान्धता सडक़ पर हिंसा का तांडव करते चलती है, और पुलिस इन पर कार्रवाई करने के बजाय इनकी सुरक्षा करते चलती है।
यह पूरा सिलसिला देश में बढ़ती हुई ऐसी धर्मान्धता, और साम्प्रदायिकता का नतीजा है, जो कि पूरी तरह बेकाबू है। जिन रेलगाडिय़ों को सबसे सुरक्षित माना जाता था, उन रेलगाडिय़ों से अब मुसाफिरों को पीट-पीटकर फेंक दिया जाता है, और जाहिर है कि ऐसी हिंसा पर कोई कारगर कार्रवाई नहीं होती, तभी मुजरिमों का इतना हौसला बनता है। यह तो चारों तरफ बिखरे हुए मोबाइल-कैमरों की मेहरबानी है कि हिंसा के सुबूत जुट ही जाते हैं, वरना कोई गिरफ्तारी भी नहीं हो पाती। लेकिन हमारा ऐसा अंदाज है कि आज देश जिस हद तक धर्मान्ध हो चुका है, साम्प्रदायिक हिंसा के मुजरिम पुलिस, जेल, और अदालत तक तरह-तरह का सम्मान ही पाते होंगे।
किसी देश या समाज में, या प्रदेश में ऐसी अराजक हिंसा को बढ़ावा देना तो आसान है, लेकिन इससे छुटकारा पाना कुछ वैसा ही मुश्किल होगा जैसा कि एक कहानी में अपने बनाए गए शेर में प्राण फूंकने के बाद उससे उतरना मुश्किल होता है, शेर खा जाता है। मुंह में खून लगने पर महज जानवर ही मानवभक्षी नहीं होते, इंसान भी एक बार हिंसा की ताकत का लहू चख लेते हैं, तो उन्हें फिर उस हिंसा का स्वाद बार-बार खींचता है, और अगली हिंसा करवाता है। किसी धर्म के ऐसे हिंसक लोग हर बार दूसरे धर्म के साथ ही हिंसा नहीं करते, जब ऐसे हिन्दू, हिन्दू बहुल आबादी में ऐसा भयानक शोर करते निकलते हैं, या किसी धार्मिक आयोजन में बेकाबू लाउडस्पीकर बजाते हैं, तो वे मोटेतौर पर हिन्दुओं का ही सुख-चैन छीनते हैं। सरकारों में ऐसी गुंडागर्दी के खिलाफ कार्रवाई के लिए बहुत बड़े हौसले की जरूरत नहीं है, जरूरत महज इतनी है कि निर्वाचित सत्तारूढ़ नेता अफसरों को कानून के हिसाब से काम करने दें।
छत्तीसगढ़ के एक नए बने जिले, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के एक स्कूल का एक वीडियो अभी सामने आया है जिसमें साल्हेवारा नाम की जगह पर स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी-हिन्दी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का समारोह चल रहा है, और 8 छात्राएँ स्कूल की पोशाक में ही मंच पर एक किसी धार्मिक गाने पर पूरे बाल खोलकर इस अंदाज में झूम रही हैं कि उन पर कोई देवी आई हो। काफी देर तक स्टेज पर वे इसी तरह झूमती दिखती हैं, और सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखने वाले लोग हैरान हैं। उनमें से कई लोग तो मामले की गंभीरता समझे बिना उस पर जोरों से हँसने के निशान पोस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग यह भी लिख रहे हैं कि सरकारी स्कूल में यह हो क्या रहा है? यह नौबत बहुत ही भयानक है। देश का संविधान नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना के विकास की जिम्मेदारी देश के तमाम तबकों पर डालता है। अब अगर इस तरह के धार्मिक अंधविश्वास अगर सरकारी स्कूलों में लड़कियों के बीच पनपाए जा रहे हैं, तो उनका असर बहुत दूर तक होगा।
हमारे पाठकों को याद होगा कि हम बार-बार देश में वैज्ञानिक चेतना में गिरावट पर फिक्र जाहिर करते आए हैं। आज दिक्कत यह हो गई है कि कहने में जिस धर्म को मासूम करार दिया जाता है, वह धर्म एक पैर धर्मान्धता पर रखे हुए खड़े रहता है। फिर भारत की लोकतांत्रिक राजनीति की बदनीयत है कि वह तुरंत ही धर्म का राजनीतिकरण करने पर उतारू हो जाती है। अगला कदम साम्प्रदायिकता और अंधविश्वास की तरफ रहता है। इसके साथ-साथ धर्म के आक्रामक तेवर उसे लोकतंत्र की सीमाओं के एकदम बाहर ले जाते हैं। फिर कहने के लिए तो भारत की औपचारिक शिक्षा विज्ञान पढ़ाती है, लेकिन जिस तरह से स्कूली बच्चों से लेकर जिंदगी के दूसरे दायरों में भी जिस हद तक धर्मान्धता भरी जा रही है, उससे जाहिर है कि बच्चों की वैज्ञानिक सोच खत्म हो रही है। दिक्कत यह है कि आज भारत विज्ञान और टेक्नॉलॉजी के तमाम फायदों का इस्तेमाल करते हुए भी जिस तरह राजनीतिक नारेबाजी में विज्ञान को खारिज करता है, इतिहास-पूर्व के जाने किस विज्ञान को सब कुछ मानता है, उससे विज्ञान की पढ़ाई पता नहीं कहां जाकर गिरेगी।
जब समाज और परिवार, सार्वजनिक जीवन, ये सब एक बहुत हाईवोल्टेज धार्मिक गतिविधियों से भरे रहेंगे, और उन धार्मिक गतिविधियों को ही इतिहास पर आधारित बता दिया जाएगा, पौराणिक कहानियों को इतिहास करार दे दिया जाएगा, तो ऐसी सोच और समझ के भरोसे बच्चों की कल्पनाओं का पुष्पक विमान 21वीं सदी के चांद और मंगल तक कैसे पहुंच पाएगा?
सरकारी स्कूलों में छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्वामी आत्मानंद स्कूलों को माना गया है, और उन्हें उसी महत्व के साथ ढाला जाता है। अब इन स्कूलों में भी आजादी की सालगिरह के मंच का कार्यक्रम छात्राओं पर धार्मिक गाने पर नाचते हुए सामूहिक रूप से देवी आने का हो रहा है, तो इससे यह समझ पड़ता है कि बच्चियों से परे भी स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य तक किस सोच के होते जा रहे हैं। यह किसी धर्म का धर्म पढ़ाने वाला स्कूल होता, तो भी बात समझ में आती, लेकिन यह तो प्रदेश में सबसे अधिक सुविधाओं वाला आत्मानंद स्कूल है जिसमें दाखिले के लिए बच्चों के बीच कड़ा मुकाबला होता है, जहां अनुपातहीन अधिक खर्च करके चुनिंदा बच्चों को अधिकतम सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं।
दुनिया के किसी भी समझदार देश में धर्म निजी आस्था का सामान रहना चाहिए। लोग अपने घरों में अपनी धार्मिक मान्यताओं पर अमल करें, अपने आस्था केन्द्रों पर जाकर वहां भी अपने रीति-रिवाज से जो करना है कर लें, लेकिन जब धर्म का विस्तार सरकारों तक हो रहा है, सरकारी स्कूल-कॉलेज तक हो रहा है, सार्वजनिक जीवन को तहस-नहस करने की हद तक सडक़ों पर हो रहा है, लाउडस्पीकरों से बाहर निकलकर नवजात बच्चों को मार डाल रहा है, तो ऐसे धर्म के बारे में लोगों को सोचना चाहिए। यह बात किसी एक धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि अलग-अलग कई धर्मों, अधिकतर या सभी धर्मों को लेकर है।
हमने कुछ दिन पहले ही मदरसों में धर्म की पढ़ाई के बारे में लिखा था कि उससे, और दूसरी जगहों पर बाकी धर्मों की पढ़ाई से, बच्चे धर्म पर पलने वाले परजीवियों की तरह बनकर रह जाते हैं, और वे आज की आधुनिक दुनिया की जरूरतों से इतने दूर चले जाते हैं कि धर्म के रहमोकरम के बिना उनकी कोई जिंदगी नहीं रह जाती। अब अगर किसी भी धर्म के ‘मदरसों’ तक जो हाल सीमित रहना चाहिए था, वह अगर सबसे महंगी, और सबसे अच्छी कही जाने वाली सरकारी स्कूलों तक बिखर जा रहा है, तो इस बारे में समाज को सोचना चाहिए। जिन लोगों को यह लगता है कि आज धर्म खतरे में है, तो धर्म पर तो हमें किसी तरह का खतरा नहीं दिखता, और जनता की वैज्ञानिक सोच जरूर पूरी तरह खतरे में है, और ऐसे समाज का भविष्य भी खतरे में है। आज देश के भीतर कामयाब जगहों पर पहुंचने वाले लोग, इस देश से निकलकर बाकी दुनिया में सफल होने वाले लोग किसी धार्मिक अंधविश्वास से सफल नहीं होते, वे असली और ईमानदार ज्ञान पाकर कामयाब होते हैं, या विज्ञान और टेक्नॉलॉजी पर और आगे की रिसर्च करके कामयाब होते हैं।
मैंने आज एक छोटी सी घटना को लेकर यह बड़ी सी फिक्र बताई है, और अगर इस घटना का ऐसा ही सिलसिला आगे बढ़ते रहा तो वह दिन दूर नहीं है जब संपन्न और ताकतवर तबके अपने बच्चों को तो धर्मान्धता से दूर रखकर देश-विदेश में सबसे उम्दा पढ़ाई मुहैया करा देंगे, और देश की बाकी जनता इसी तरह सिर धुनती रह जाएगी।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
बीते जमाने के एक बड़े चर्चित और प्रमुख फिल्म-पत्रकार के फेसबुक पेज पर आज सुबह उनकी दो बच्चों के साथ की एक तस्वीर दिखाई दी, जिसमें एक छोटा लडक़ा एक टी-शर्ट पहने हुए है जिस पर एक लाईन छपी है, नेटफ्लिक्स, एंड अवॉइड पीपुल। मतलब यह कि नेटफ्लिक्स को देखो, और इंसानों से परहेज करो। बाद में इस नारे को लेकर जब टी-शर्ट बाजार को ऑनलाईन देखा गया, तो समझ आया कि यह टी-शर्ट आम है, और मजाकिया अंदाज में लिखा गया यह स्लोगन लोगों को इंसानों से दूर रहकर फोन या टीवी की स्क्रीन में डूब जाने की सलाह देता है। कहने के लिए तो यह एक आम बाजारू प्रचार है, लेकिन जो लोग सचमुच ही किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म, किसी सोशल मीडिया, या किसी डिजिटल एप्लीकेशन के शिकार होकर उसमें डूब जाते हैं, उनका क्या हाल होता है?
पिछले कुछ दिनों से हर सुबह बीबीसी वल्र्ड न्यूज के जो पॉडकास्ट मैं सुनता हूं, उसमें उन्हीं के किसी एक दूसरे प्रोग्राम का प्रचार भी सुनाई पड़ता है जो कहता है कि दुनिया में आज सबसे बड़ा डिजाइनर नशा डिजिटल शक्ल में है, और उन्हें बनाने वाले लोग जैसा चाहते हैं, इस नशे के शिकार लोग ठीक वैसा ही करते हैं। इस प्रोमो के शब्द कुछ आगे-पीछे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यही है कि इंसान के गढ़े हुए सबसे घातक और असरदार नशे के सामान प्रयोगशाला में बनाया गया नशा नहीं है, बल्कि वह डिजिटल एप्लीकेशन या प्रोग्राम हैं जो कि लोगों को बांध लेते हैं। लोगों को याद होगा कि अभी कुछ हफ्ते पहले ही पूना में एक मोबाइल गेम खेलते हुए 14 बरस का एक लडक़ा उस खेल की चुनौती को मंजूर करके 14वीं मंजिल से कूद गया था, और नीचे जमीन से टकराते ही उसकी मौत हो गई थी।
लोगों को याद होगा कि ऐसी घातक चुनौतियां पेश करने वाले कुछ खेलों को हिन्दुस्तान में पिछले बरसों में रोक दिया गया है, और सरकार ने टिक-टॉक जैसे कुछ और बहुत लोकप्रिय मोबाइल ऐप भी कुछ दूसरी वजहों से यहां रोक दिए हैं, क्योंकि उन पर चीन की तरफ से जासूसी करने का शक पूरी दुनिया में किया जाता है। अमरीका में भी यह एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि टिक-टॉक को मार दिया जाए, या छोड़ दिया जाए?
हम इन दिनों मोबाइल फोन के कई तरह के प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को देखते हैं, तो लोग वहां अपनी रील बनाकर डालते हुए बावले से हो जाते हैं। कोई किसी इंजन की छत पर चढक़र मोबाइल फोन से एक खतरनाक रिकॉर्डिंग करते हुए बिजली के तारों में जलकर मर जाते हैं, कुछ लोग कारों सहित नदी में गिरकर डूब जाते हैं, और कई लोग सडक़ों पर खतरनाक ड्राइविंग के वीडियो की लाईव स्ट्रीमिंग करते हुए मारे जाते हैं।
दस-बीस बरस तक इनमें से कोई भी शौक लोगों के पास नहीं था, मोबाइल फोन आ भी गए थे तो भी ऐसी रिकॉर्डिंग करके उसे नेट पर डालने, या मैसेंजरों से फैलाने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। लेकिन हाल के बरसों में लोगों को मोबाइल फोन और ऐप का यह ऐसा मिलाजुला हथियार हाथ लगा है कि उससे वे अपने दिमागी सुख-चैन का भी कत्ल कर रहे हैं, और परिवारों के भीतर भी रिश्ते टूट रहे हैं। नाबालिग बच्चों से लेकर शादीशुदा महिलाओं तक जाने कितने किस्म की खुदकुशी सामने आती हैं जिनमें मोबाइल फोन न मिलने पर जिंदगी ही खत्म कर दी गई है। लोग अपने चेहरे, अपने फैशन, अपनी सही-गलत हरकतों को सोशल मीडिया पर डालने के लिए भयानक दर्जे के बावले हो रखे हैं। और तो और अलग-अलग शहरों के गुंडे-मवालियों के गिरोह भी अपने हथियारों की नुमाइश करते हुए सोशल मीडिया पर अपने वीडियो पोस्ट करते हैं, ताकि उनकी रंगदारी पर लोग दहशत में जल्दी आएं।
कई किस्मों से मोबाइल और कम्प्यूटर सरीखे हार्डवेयर ने, और अलग-अलग एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर ने लोगों को वैसे भी अपनी असल जिंदगी से काट दिया है, और ऑनलाईन दुनिया के बाशिंदे बना दिए हैं। लोगों को ऑनलाईन दोस्ती और मोहब्बत असल जिंदगी के अपने दायरे के लोगों के मुकाबले अधिक सुहाने लगी हैं। ऐसे में अगर किसी टी-शर्ट पर यह सुझाव मिलता है कि वे नेटफ्लिक्स ही देखते रहें, और इंसानों से परहेज करें, तो यह समाज को जापान की मौजूदा हालत की तरफ ले जाने की एक हरकत है जहां पर लोग जिंदगी के हर काम ऑनलाईन करने के ऐसे आदी हो गए हैं कि उन्हें असल इंसानों से रूबरू मिलने में डर लगने लगा है कि वैसे रिश्ते उनसे निभेंगे कैसे?
दरअसल डिजिटल और ऑनलाईन दुनिया लोगों को एक किस्म के आत्ममोहन में जीने का मौका देती है। इस हद तक कि अब ढेर सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो लोगों को हजारों गुना अधिक सुंदर बनाकर पल भर में उनकी तस्वीर पेश कर देते हैं, और लोग उन्हें फटाफट सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर देते हैं। ऐसी सहूलियत किसी से असल जिंदगी में रूबरू होने पर हासिल नहीं रहती है। असल जिंदगी को अधिक खुशनुमा बनाने के एप्लीकेशन पूरी जिंदगी की कड़ी मेहनत से जरा सी हद तक हासिल हो पाते हैं, इसलिए लोग डिजिटल दुनिया में अपने को अधिक सुरक्षित महसूस करने लगे हैं, और फिर नेटफ्लिक्स सरीखे ओटीटी प्लेटफॉर्म तो पूरी तरह से एकतरफा हैं, और वे हर दिन इतना कुछ नया-पुराना पोस्ट करते रहते हैं कि उस सबको देखने में लोगों को कई-कई दिन लग जाएं।
जैसा कि बीबीसी का प्रोमो कहता है कि आज सबसे अधिक खतरनाक नशा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का, डिजिटल प्रोग्राम और एप्लीकेशन बनाने वाले लोगों का बनाया हुआ है, और वे लोगों के जैसे बर्ताव के लिए इन्हें बनाते हैं, लोग ठीक वैसा-वैसा बर्ताव करने लगते हैं। यह प्रोमो कहता है कि लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे डिजिटल औजारों का अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, न कि अपने आपको डिजिटल औजारों द्वारा इस्तेमाल करने दें।
डिजिटल नशामुक्ति अभी जमीन पर सब जगह हासिल नहीं है, लेकिन लोगों को बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के स्क्रीन-टाईम पर सोचने की जरूरत है। आज बहुत से बड़े लोग भी देर रात आंखें बंद हो जाने तक तरह-तरह की मादक, उत्तेजक, और अश्लील रील देखते हुए झपकी लेते रहते हैं, इस सिलसिले को तोडऩे और रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर कम से कम बात तो शुरू करनी चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
फिलीस्तीन पर इजराइल के हमलों के बीच फिलीस्तीन के हिमायती लेबनान के हथियारबंद संगठन हिजबुल्ला, यमन से इजराइली जहाजों पर हमला करने वाले एक और हथियारबंद संगठन हूथी, और इनके पीछे बताए जा रहे ईरान तक अब इजराइली हमलों का विस्तार हो चुका है। अभी दो दिन पहले उसने कुछ घंटों के भीतर ही लेबनान में हिजबुल्ला के सबसे बड़े कमांडर को मार गिराया, और ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में पहुंचे हुए फिलीस्तीनी हमास के मुखिया, और गाजा में प्रधानमंत्री रहे हुए इस्माइल हानिया को मार डाला। इसके साथ ही अब इजराइल पर ईरानी जवाबी हमले की आशंका को देखते हुए अमरीका ने अपनी बड़ी फौज उसे बचाने के लिए तैनात की है। ऐसा लगता है कि एक शहर गाजा पर इजराइल की चल रही फौजी कार्रवाई एक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकती है, जिसमें अमरीका अपनी पूरी फौजी ताकत के साथ शामिल हो सकता है।
अब अमरीका की पूरी दुनिया में मौजूदगी को देखें तो यह बात साफ दिखती है कि रूस-यूक्रेन के बीच चल रही जंग में नाटो देशों की तरफ से अगुवाई करते अमरीका ने जिस तरह यूक्रेनी सैनिकों की जिंदगी दांव पर लगवाकर रूस की फौजी और आर्थिक ताकत को खोखला करने की कोशिश की है, कुछ उस तरह की कोशिश उसकी मध्य-पूर्व के इलाके में ईरान को खोखला करने के लिए भी हो सकती है। आज अगर अमरीकी फौजी ताकत के साथ इजराइल अपनी खुद की फौजों को लेकर ईरान से जंग के किसी मोर्चे पर आमने-सामने रहता है, तो इससे ईरान पर कुछ उसी तरह की चोट पड़ सकती है, जैसी कि अमरीकी कोशिशों के बावजूद भी रूस पर नहीं पड़ सकी। जिस तरह यह माना जा रहा है कि यूक्रेन के मोर्चे पर फौजी और आर्थिक मदद करके नाटो देश एक प्रॉक्सीवॉर लड़ रहे हैं, और रूस को भविष्य के किसी मोर्चे की नौबत आने के हिसाब से खोखला कर रहे हैं, कुछ वैसा ही खोखला ईरान को करने की चाहत अमरीका और इजराइल दोनों की लंबे समय से रही है। और जहां तक प्रॉक्सीवॉर की बात है, तो ईरान भी इजराइल के खिलाफ हमास, हिजबुल्ला, और हूथी के कंधों पर बंदूक रखकर प्रॉक्सीवॉर चला ही रहा है।
इस जटिल अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में यह भी समझने की जरूरत है कि आज अमरीका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बना हुआ चीन यूक्रेन के मोर्चे पर पूरी तरह रूस के साथ है, और वह कुछ कम हद तक मध्य-पूर्व में ईरान के साथ हमदर्दी रखेगा, क्योंकि ईरान भी रूस के साथ गठजोड़ करते हुए अमरीका के खिलाफ है। इसलिए आज जो चीन सीधे-सीधे न तो यूक्रेन के मोर्चे पर फौजी लड़ाई में शामिल है, न ही वह ईरान-इजराइल मोर्चे में सीधे शामिल होगा, लेकिन इन दोनों ही मोर्चों पर अमरीकी हितों के खिलाफ चीन की सक्रियता, अमरीका की परेशानी का सबब तो होगा ही। इन दिनों दुनिया में जंग और कारोबार के मोर्चों में एक बड़ा जटिल अंतरसंबंध रहता है। चीन ने रूस को कोई फौजी मदद नहीं दी, लेकिन उसे आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा रखने के लिए उसने सब कुछ किया। मध्य-पूर्व के देशों में अभी हाल में ही चीन ने अपनी बड़ी दखल दर्ज कराई, जब उसने बरसों की मेहनत के बाद सऊदी अरब और ईरान के बीच रिश्ते कायम करवाए। इस कामयाबी और नए गठबंधन में चीन ने अपनी जमीन पर बैठे-बैठे इन दोनों के रिश्ते सुधरवाए, और इनके बीच कूटनीतिक संबंध कायम हुए। इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौते के बाद चीन का इस इलाके में एक नया महत्व कायम हुआ है।
आने वाली दुनिया में देशों और गठबंधनों के बीच जो नई व्यवस्था बनेगी, और नए रिश्ते कायम होंगे, उनमें अपनी सरहदों से परे इस तरह की मध्यस्थता का अपना एक बड़ा महत्व रहेगा, और इसमें चीन की एक कामयाबी के बाद कोई और कामयाबी उसे विश्व स्तर के एक बड़े खिलाड़ी का दर्जा दिला देगी। ऐसा लगता है कि इजराइल के कई तरफ खुल चुके मोर्चों में अमरीका इजराइल का परंपरागत साथ तो दे ही रहा है, उसके साथ-साथ वह मध्य-पूर्व में एक प्रॉक्सीवॉर खड़ा करने, और उसके नफे-नुकसान पर भी जरूर सोच रहा होगा। अफगानिस्तान में उसकी फौज और सरकार को जैसी भयानक शर्मनाक शिकस्त मिली है, उससे भी अमरीकी अहंकार तिलमिलाया हुआ होगा, और हो सकता है कि परमाणु हसरतों को पालने वाले इराक को कमजोर करने की अमरीकी हसरत भी इजराइल के बहाने पूरी हो रही हों। शायद यह भी एक वजह रही कि अमरीका एक तरफ तो लगातार इजराइल को युद्धविराम की नसीहतें देने का नाटक करते रहा, मलबा और कब्रिस्तान बन चुके गाजा पर फूडपैकेट गिराते रहा, और इसके साथ-साथ वह इजराइल को इतनी हथियार देते रहा, इतने बम देते रहा कि जिनसे हर फिलीस्तीनी को दस-दस बार मारा जा सके।
इसलिए आज इजराइल के तनाव को महज क्षेत्रीय तनाव मानकर चलना गलत होगा। ईरान के रहते इजराइल की फौजी हिफाजत की कोई गारंटी हो नहीं सकती, इसलिए भी शायद इजराइल को यह पसंद आ रहा हो कि फिलीस्तीन पर अपने जुल्म ढहाने के बाद वह उसमें मददगार अमरीका को लेबनान, यमन, और ईरान तक भी घसीटे। अमरीका को अपने परंपरागत दुश्मन, रूस, चीन, और ईरान से निपटने का एक मौका भी इजराइल की शक्ल में मिलता है, और इन तीनों देशों की फौजी ताकत को घटाना, अमरीका को एक सस्ता सौदा लग सकता है। उधर उसे प्रॉक्सीवॉर के लिए यूक्रेन मिला, और इधर इसी काम के लिए उसे इजराइल हासिल है। देखना है कि अपनी जमीन पर ऐसा अपमान झेलने के बाद ईरान किस तरह की जवाबी फौजी कार्रवाई करता है, और अमरीका इस मोर्चे पर किस हद तक शामिल होता है।
एमपी के रीवां की खबर है कि एक गांव में तीन महीने पहले 9 बरस की एक बच्ची से रेप के बाद उसका कत्ल करने वाला उसका 13 बरस का सगा भाई ही था। जांच के बाद, डीएनए टेस्ट के बाद पुलिस ने अभी इस लडक़े को उसकी मां और दो बहनों के साथ गिरफ्तार किया है। नाबालिग भाई-बहन को सुधारगृह भेजा गया है, और मां और एक बालिग बहन को जेल भेजा गया है। पुलिस ने जांच के नतीजे बताए हैं कि 13 बरस का यह लडक़ा मोबाइल पर पोर्न वीडियो देखा करता था। एक रात उसने पोर्न वीडियो देखने के बाद अपने पास सो रही छोटी बहन के साथ बलात्कार किया। जब बहन ने यह बात पिता को बताने की धमकी दी, तो उसने 9 बरस की बहन को गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद उसने मां को जगाकर सब बताया, फिर मां और दो बहनों ने मिलकर सारे सुबूत खत्म किए, और पुलिस को कहा कि कोई अनजान व्यक्ति ऐसा कर गया है। लेकिन लडक़ी के बदन से मिले डीएनए सेम्पल की जांच से मुजरिम भाई के ही होने के सुबूत मिले, और पुलिस ने एक परिवार के ही इन चार लोगों को गिरफ्तार किया, दो लोग सुधारगृह और दो लोग जेल भेजे गए। छोटी सी बेकसूर लडक़ी बलात्कार और कत्ल से गुजर ही गई। किसी परिवार के साथ इससे बड़ी तबाही और क्या हो सकती है? और सोचने की बात यह है कि यह सिलसिला शुरू कहां से हुआ?
हिन्दुस्तान में किशोरावस्था में पहुंचे लडक़े-लड़कियों के लिए सेक्स की जानकारी पाने का अकेला जरिया पोर्न वीडियो ही रहते हैं। इन दिनों दस बरस के बच्चों को भी ऐसे वीडियो कहीं न कहीं मिल जाते हैं, और जिनके हाथ मोबाइल फोन, लैपटॉप या कम्प्यूटर लग जाते हैं, उनकी पहुंच तो दुनिया के सबसे हिंसक वयस्क वीडियो तक हो जाती है। हालत यह है कि लोग छोटे बच्चों के सेक्स के वीडियो भी एक-दूसरे को भेजते रहते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं, और हर हफ्ते हम अपने आसपास ऐसी गिरफ्तारियां देखते हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय निगरानी एजेंसियों की भेजी जानकारी के आधार पर होती हैं, वहां से जानकारी भारत सरकार को आती है, और यहां पर सरकार उसे प्रदेशों में भेजकर बच्चों के पोर्न अपलोड या पोस्ट करने वाले लोगों को गिरफ्तार करती हैं। जो लोग बालिग हो चुके हैं, उन्हें भी नाबालिग लोगों के पोर्न वीडियो पोस्ट न करने की जिम्मेदारी समझ में नहीं आती, क्योंकि उन्हें देह और सेक्स की जानकारी कभी वैज्ञानिक तरीके से दी नहीं गई, और वे सिर्फ पोर्न वीडियो के रास्ते ग्रेजुएशन हासिल करने वाले लोग रहते हैं। उन्हें यह भी समझ नहीं पड़ता कि नाबालिगों के सेक्स की फोटो या उसका वीडियो आगे बढ़ाना जुर्म के दायरे में आता है।
आज 13 बरस का एक लडक़ा घर के भीतर 9 बरस की सगी बहन से बलात्कार कर रहा है, और उसे बलात्कार की जानकारी और उसकी प्रेरणा पोर्न वीडियो से मिल रही है। जबकि उसकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि स्कूल में उसकी देह और सेक्स की जिज्ञासा का जवाब वैज्ञानिक जानकारियों के साथ शिक्षकों द्वारा सरल तरीके से दिया जाना चाहिए था, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है। लोग भारत की एक काल्पनिक ऐतिहासिक परंपरा और संस्कृति का हवाला देते हुए प्रेम और सेक्स के इतने खिलाफ हो गए हैं कि आज कृष्ण के लिए भी गोपियों के साथ रास रचाना मुमकिन नहीं हो पाता। कहीं नदी किनारे, तो कहीं पेड़ों के नीचे कृष्ण की रासलीला की जो तस्वीरें भारत में सैकड़ों बरस से प्रचलित हैं, जिनका बड़ा बखान संस्कृत से लेकर लोकभाषाओं और बोलियों तक में मिलता है, वह आज लाठी खाने लायक काम मान लिया जाता।
एक काल्पनिक और पूरी तरह से झूठी तस्वीर भारत की पुरानी संस्कृति की बनाई गई है जिसका हकीकत से कोई लेना-देना नहीं रहा, और नई पीढ़ी को अपनी देह को समझने से पूरी तरह दूर रखा जाता है। यही वजह है कि बच्चे अपनी जानकारी ऐसे हिंसक और क्रूर पोर्न वीडियो से पाते हैं, जो कि असल जिंदगी का सेक्स भी नहीं बताता। वह सेक्स के मामले में गब्बर सिंह सरीखे एक काल्पनिक किरदार को खड़ा करता है, और न सिर्फ बच्चों, बल्कि हिन्दुस्तानी बालिग लोगों के दिमाग में भी सेक्स की ऐसी कल्पना भर देता है जो कि असल जिंदगी में कभी पूरी नहीं होती। पोर्न फिल्मों के कैमरों के सामने पेशेवर चुनिंदा किस्म के वयस्क कलाकार, कई किस्म की दवाईयों की मदद से सेक्स की जो शक्ल सामने रखते हैं, वहीं से उसके दर्शकों के दिमाग में सेक्स का एक बहुत ही हिंसक रूप बैठ जाता है। और नाबालिग लोगों या छोटे बच्चों के दिमाग में तो यह हिंसक किस्म का प्रायोजित और नाटकीय सेक्स तूफान ही ला देता है।
कुछ बरस ही हुए हैं जब छत्तीसगढ़ के एक परिवार में एक छोटी लडक़ी से, उसी के तीन-चार भाईयों ने गैंगरेप किया था, और परिवार इस दुविधा में पड़ गया था कि सच्ची रिपोर्ट लिखाने से घर के सारे बच्चे सुधारगृह चले जाएंगे, तो रिपोर्ट लिखाई जाए, या नहीं?
फिलहाल इस घटना की चर्चा इसलिए जरूरी है कि तथाकथित भारतीय संस्कृति के फतवों से नौजवान पीढ़ी का दिल-दिमाग विकसित नहीं होता, उसके लिए उन्हें अपनी उम्र के मुताबिक जानकारी दी जानी चाहिए। सत्तारूढ़ पार्टी के लिए यह एक अलोकप्रिय बात हो सकती है कि स्कूलों में सेक्स-शिक्षा या देह-शिक्षा देने का फैसला उसके नाम संग जोड़ा जाए। राजनीतिक दल इससे कतराते रहेंगे। दूसरी तरफ आज के वक्त की बच्चों की पीढ़ी की शारीरिक और मानसिक, भावनात्मक, और सामाजिक जरूरतों को देखते हुए स्कूलों का पाठ्यक्रम बनाने का जिम्मा जिन जानकार विशेषज्ञों पर होना चाहिए, उनकी बजाय वोटों के गलाकाट मुकाबले में लगे हुए नेता यह फैसला लेने लगे हैं। बच्चों की शिक्षा-दीक्षा एक बहुत ही विशेषज्ञता वाला काम है, और उसे हिन्दुस्तान में एक लुभावनी राजनीतिक घोषणा का सामान बना लिया गया है, नेता आमसभाओं के मंच से माईक पर पाठ्यक्रम तय करते हैं, और यह अंदाज देखकर दुनिया के विकसित देश हक्का-बक्का रह सकते हैं, जहां पढ़ाई में नेताओं की कोई दखल नहीं होती। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
हिन्दुस्तानी सुप्रीम कोर्ट अभी एक दिलचस्प मामले पर गौर कर रहा है कि भारत के राज्यपालों को आपराधिक मुकदमों से मिली सुरक्षा जायज है या नहीं। हम बरसों से इस बात को लिखते आ रहे हैं कि संविधान में राज्यपालों को दी गई हिफाजत की रियायत अलोकतांत्रिक है। अभी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी.आनंद बोस के खिलाफ राजभवन की एक महिला कर्मचारी द्वारा यौन शोषण की शिकायत को लेकर पहुंचा है। संविधान में धारा 361 में राज्यपाल को पद पर रहने तक किसी भी आपराधिक मामले से छूट मिली हुई है। इसलिए बंगाल पुलिस महिला की एफआईआर पर भी राज्यपाल पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। लेकिन हम देश में कई दूसरे राज्यपालों की मिसालें भी देखें तो भी यह समझ पड़ता है कि आज के वक्त राज्यपालों का जो हाल रहता है उसमें ऐसी अंधी रियायत देना ठीक नहीं है। दूसरे भी कई राज्यपाल ऐसे हुए हैं जो कि बड़े-बड़े आपराधिक मामलों में फंसे रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मध्यप्रदेश में 2015 में भयानक विशाल पैमाने के व्यापमं घोटाले में वहां के उस वक्त के राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ विशेष जांच दल ने सुबूत पाए थे। उनके बेटे शैलेष यादव को भी भर्ती घोटाले में शामिल पाया गया था। उनके ओएसडी धनराज यादव को गिरफ्तार भी किया गया था। अपने खिलाफ मामला देखकर राज्यपाल हाईकोर्ट गए थे कि संविधान के हिसाब से पद पर रहने तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, और अदालत ने रामनरेश यादव की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, लेकिन जांच जारी रखने की छूट दी थी। जांच दल के मुखिया ने कहा था कि यादव के रिटायरमेंट के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन शायद वे ऐसी नौबत आने के पहले गुजर ही गए थे। यह मामला इतना भयानक था कि इसमें एमपी के बड़े भाजपा नेता और राज्य के मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की भी गिरफ्तारी शिक्षक भर्ती घोटाले में हुई थी।
संविधान में राज्यपाल की चाहे जो भी भूमिका बनाई गई हो, उसे किसी तरह की अलोकतांत्रिक हिफाजत देना बहुत ही नाजायज है। इसका मतलब तो यह है कि जिन बातों को लेकर एक छोटे कर्मचारी को तुरंत जेल में डाला जा सकता है, उससे हजार गुना बड़ा जुर्म करके भी राज्यपाल या राष्ट्रपति जैसे लोग बच सकते हैं। यह परले दर्जे की शर्मिंदगी की बात है कि जांच में कुसूरवार दिखने पर भी राज्यपाल अपने संवैधानिक ओहदे को छोडक़र घर नहीं बैठते, बल्कि कुर्सी पर चिपके रहकर गिरफ्तारी से बचने के लिए एक पेशेवर मुजरिम की तरह अदालत दौड़ते हैं। कुछ लोगों को अपनी ऊंची और विशेषाधिकार से लैस कुर्सी की इज्जत का ख्याल भी नहीं रहता, बस उससे चिपके रहकर, तरह-तरह के जुर्म करके कमाने या मजा लेने की ही सूझती है।
मैं लंबे समय से राज्यपाल की व्यवस्था के ही खिलाफ लिखते आ रहा हूं। मेरा मानना है कि राजभवन की व्यवस्था पूरी तरह गैरजरूरी, अलोकतांत्रिक, राजनीतिक-साजिश की, और खर्चीली है। दुनिया के बहुत से लोकतंत्र बिना ऐसे राज्यपाल के चलते हैं, और उनका कोई भी काम नहीं रूकता। हिन्दुस्तान में तो राजभवनों को राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने, विधायकों की खरीद-फरोख्त की मंडी चलाने, भ्रष्टाचार करने, और निर्वाचित लोकतांत्रिक ताकतों को कमजोर करने के लिए नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता है। जाने कितने ही राज्यपालों को सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर झिडक़ चुका है, और महाराष्ट्र सरीखे राज्य में तो एक वक्त राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष इन दोनों के बीच यह मुकाबला चल रहा था कि केन्द्र सरकार को अधिक खुश कौन कर सकता है। अब जब राज्यों में निर्वाचित विधायकों की चुनी गई सरकार बिल्कुल साफ-साफ चलनी चाहिए, तो उसमें केन्द्र सरकार की राजनीतिक एजेंट की तरह राज्यपाल साजिश में जुट जाएं, यह लोकतंत्र को कमजोर और खोखला करने के अलावा और कुछ नहीं है। फिर अलग-अलग समय पर अलग-अलग प्रदेशों के राज्यपाल भ्रष्टाचार में भी फंसे रहे, निर्वाचित सरकार के काम में अड़ंगे लगाते रहे, और कुछ राजभवन तो सेक्स के मजे का अड्डा भी बने रहे। लोगों को शायद होगा कि किस तरह एक बहुत बुजुर्ग हो चुके राज्यपाल के सेक्स-वीडियो हैदराबाद के राजभवन से निकलकर चारों तरफ फैले थे, और एक उच्च-सवर्ण बुजुर्ग की रवानगी का सामान बने थे। भारत में ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के जुर्म करने पर धर्म या जाति की कोई व्यवस्था आड़े नहीं आती, बल्कि मुजरिमों का एक जातिविहीन, सर्वधर्म समाज अलग ही नजर आता है।
सुप्रीम कोर्ट शायद राज्यपाल की संवैधानिक व्यवस्था पर सुनवाई करने का हकदार नहीं है, लेकिन राज्यपाल को किसी भी जुर्म के मामले में मिले हुए संरक्षण के खिलाफ सुनवाई का हक तो उसे है ही। लोकतंत्र में ऐसी कोई भी रियायत किसी को नहीं मिलनी चाहिए। जिस वक्त ऐसी रियायत का इंतजाम संविधान में किया गया होगा, उस वक्त लोगों को पता नहीं होगा कि एक दिन ऐसा आएगा, जब राज्यपाल अपनी आल-औलाद सहित राज्य की नौकरियों को बेचने का धंधा करेंगे, कॉलेजों की सीट बेचेंगे, महिला कर्मचारियों को दबोचेंगे, और उनके सेक्स के वीडियो लोगों का वयस्क मनोरंजन करेंगे। अब जब लोकतंत्र की इतनी दुर्गति हो चुकी है, और राज्यपाल बहुत से राज्यों में केन्द्र से सुपारी लेकर लोकतांत्रिक-संवैधानिक व्यवस्था की हत्या के लिए भाड़े के हत्यारे की तरह काम करने लगे हैं, तो ऐसे मुजरिमों को पूरे कार्यकाल तक मुकदमे से रियायत क्यों दी जाए? ममता बैनर्जी चाहे राज्यपाल के खिलाफ ही क्यों न रहती आई हो, क्या उस वजह से राजभवन की महिला कर्मचारी को अपने देहशोषण के खिलाफ आवाज उठाने का हक गंवाना पड़ेगा? और जब यह बेशर्म राज्यपाल मीडिया के सौ चुनिंदा लोगों को इकट्ठा करके राजभवन के सीसीटीवी कैमरों की चुनिंदा रिकॉर्डिंग दिखाकर, उनमें उस महिला को दिखाकर अपने को बेकसूर साबित करने का काम कर सकता है, तो यही काम वह अदालत के कटघरे से करे। इस देश में ऊंचे ओहदे पर बैठे एक आदमी का ऐसा हक कैसे हो सकता है कि उसके जुल्म के खिलाफ एक आम नागरिक को इंसाफ पाने का हक न रह जाए? अगर किसी वक्त मासूमियत और नासमझी से ऐसी संवैधानिक व्यवस्था की भी गई थी, तो राज्यपालों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यह व्यवस्था खत्म करनी चाहिए। हो सकता है कि यह संवैधानिक-हिफाजत खत्म होने से बहुत से राज्यपालों का जुर्म करना कम हो जाएगा। आज तो यह हिफाजत राज्यपालों को मुजरिम बनने का एक असाधारण हौसला देती है, यह लोकतंत्र की किस भावना का सम्मान है? देश के राजभवनों में महिलाओं की हिफाजत के लिए भी यह जरूरी है कि राज्यपालों के खूनी पंजों को भी हथकड़ी के दायरे में लाया जाए।
हर कुछ महीनों में यह दिखाई देता है कि कहां कौन सा नया तालाब सरकारी अवैध कब्जे और अवैध निर्माण का शिकार हो रहा है। देश भर में तालाबों के किनारे गरीबों के अवैध कब्जे तो होते ही रहते हैं क्योंकि उन्हें बसने के लिए जगह की हमेशा कमी रहती है, लेकिन जब स्थानीय म्युनिसिपल या राज्य शासन या बड़े कारोबारी तालाबों के किनारे अवैध कब्जा और अवैध निर्माण करते हैं तो वह जिंदगी गुजारने के लिए मजबूरी का कोई काम नहीं रहता, वह कमाई करने के लिए किया जा रहा गैरकानूनी काम रहता है।
छत्तीसगढ़ में लगातार यह छपते ही रहता है कि किस जगह नगर निगम तालाब के किनारे पाल बनाने के नाम पर, रास्ता बनाने के नाम पर तालाब के कुछ हिस्से को पाटने पर आमादा है, और सौंदर्यीकरण के नाम पर अंधाधुंध पैसा भी झोंका जा रहा है, और पानी की जगह कम की जा रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के अनगिनत फैसले सामने हैं जो कहते हैं कि किसी भी तरह की पानी की कोई सार्वजनिक जगह, कोई सार्वजनिक मैदान या उद्यान, या कोई चारागाह खत्म न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे भी फैसले हैं कि अगर इनमें से किसी जगह पर कोई पक्का निर्माण हो भी चुका है, तो भी उसे हटाकर उसे उसके मूल सार्वजनिक स्वरूप में वापिस लाया जाए, यानी अगर तालाब के किसी हिस्से को पाटकर वहां किसी तरह का निर्माण किया गया है, तो उसे तोडक़र फिर से तालाब बनाया जाए, या चारागाह अगर निर्माण में खत्म हो रहा है, तो ऐसे निर्माण तोड़े जाएं।
हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को एक मिसाल के तौर पर लेते हैं क्योंकि यहां की खबरों को कुछ अधिक करीब से देखते हैं। मौजूदा और पुराने शहर रायपुर से लेकर नए बसे हुए कॉलोनीनुमा शहर नया रायपुर तक अनगिनत तालाब ऐसे हैं जिन्हें खूबसूरत बनाने के नाम पर म्युनिसिपल से लेकर पर्यटन विभाग तक, और स्मार्टसिटी प्रोजेक्ट तक के करोड़ों रूपए झोंके जा रहे हैं, और उनकी पानी की जगह सिमटती जा रही है। कुछ ऐसा ही शहर के बगीचों के साथ हो रहा है, और खेल के मैदानों के साथ तो हो ही चुका है। इन सबके पीछे सबसे बड़ी नीयत कंस्ट्रक्शन में होने वाली मोटी काली कमाई की रहती है, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो वह पैसा कैसे मिलेगा? इसलिए हर खुली जगह पर कुछ न कुछ बनाने की एक हिंसक कार्रवाई चलती रहती है। हमने अनगिनत तालाबों, बगीचों, और मैदानों को इसी तरह सिमटते देखा है। जब कभी ऐसे किसी निर्माण या तथाकथित सौंदर्यीकरण को लेकर हल्ला उठता है, तो एकाएक म्युनिसिपल, स्मार्टसिटी, या पर्यटन विभाग किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह अनजान बन जाते हैं, और इस काम की जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालने लगते हैं। हालत तो यहां तक बिगड़ी हुई है कि शहर के बीचों-बीच किसी डिवाइडर को मोटी रकम लगाकर फाइबर के पैनलों से ढांका जा रहा था, और जब यह विवाद उठा कि इसका तो टेंडर ही नहीं हुआ है, तो म्युनिसिपल ने यह कह दिया कि वह इस काम को करवा ही नहीं रहा है, और इसका जिम्मा किसी व्यापारी संगठन पर डाल दिया गया, मानो व्यापारी संगठन सडक़ पर अपनी मर्जी से इतना बड़ा कोई काम कर सकता है, और म्युनिसिपल उससे अनजान रह सकता है।
यह समझने की जरूरत है कि सरकारी संस्थाओं की अतिसंपन्नता कुदरत को खत्म करने की सुपारी उठा चुकी है। छत्तीसगढ़ में शहरों पर खर्च करने के लिए सरकार के पास इतना अधिक पैसा है कि किसी अच्छे-भले फुटपाथ को उखाडक़र उसे दुबारा बनाया जाता है, जिस पर न पहले कोई चलते थे, और न दुबारा बनाने के बाद कोई चलेंगे। सरकार के जितने भी किस्म के विभाग और दफ्तर हो सकते हैं, वे बहुत तेजी से बजट और दूसरे किस्म की रकम को खर्च करने की हड़बड़ी में रहते हैं, और ऐसा लगता है कि उन्होंने कम से कम समय में अधिक से अधिक खर्च करने की कोई शर्त लगाई हुई है। हमें सरकारी या म्युनिसिपल निर्माण के भ्रष्टाचार की उतनी फिक्र नहीं है जितनी फिक्र तालाबों पर गैरजरूरी निर्माण करके पानी के इलाके को घटाने की हरकत से है। यह सिलसिला बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, अफसरों और नेताओं को अलग कोई जमीन आबंटित कर देनी चाहिए जहां पर वे तरह-तरह के फर्जी निर्माण करवा सकें, और उसमें कमाई कर सकें।
जनता के बीच का भी कोई जागरूक तबका रहता, तो वह तालाब जैसी जरूरी और जीवन-रक्षक सार्वजनिक-धरोहर को बचाने के लिए अदालत तक गया रहता, लेकिन अभी तो हमें इस प्रदेश में ऐसे लोग दिखते नहीं हैं, जबकि ऐसे नाजायज निर्माण की खबरें लगातार छपती हैं। अब तो यही लगता है कि प्रदेश के हाईकोर्ट को अपने ऐसे न्याय-मित्र नियुक्त करने चाहिए जो कि प्रदेश भर की खबरों को लेकर रोजाना ही अदालत के सामने नियमों को तोडऩे की लिस्ट पेश कर सके, और फिर अदालत के कहे मुताबिक इनमें से छांटे गए मामलों की जानकारी सरकार से मंगा सके, और जरूरत लगे तो अदालत इन पर खुद होकर मुकदमा शुरू कर सके। इससे कम में हमें तालाब बचते नहीं दिखते हैं। हाईकोर्ट को भी तालाबों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख के बाद के तमाम मामलों को देखना चाहिए क्योंकि धरती पर तालाब सिर्फ देखने के लिए नहीं है, उनसे जमीन के नीचे का पानी भी जुड़ा हुआ है, और अगर तालाब घटते चले गए, तो भूजल का स्तर गिरते चले जाएगा। अब तो हालत यह हो गई है कि कोई बड़ा बिल्डर किसी इलाके में अपना कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाता है, तो आसपास के तालाबों को सौंदर्यीकरण के नाम पर सरकारी खर्च से पटवाना भी शुरू कर देता है, कहीं वह गैरजरूरी चौड़ी सडक़ बनवा देता है, ताकि उसके प्रोजेक्ट का बाजारू महत्व बढ़े, तो कहीं वह तालाबों के आसपास लोगों के टहलने के नाम पर उसे चारों तरफ से पटवाता है ताकि उसके अपने प्रोजेक्ट के खरीददार वहां घूम सकें। यह सिलसिला हाईकोर्ट की दखल के बिना रूकते नहीं दिखता है।
अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में बाकी तमाम मुद्दों के साथ-साथ एक मुद्दा यह भी बना हुआ है कि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन को क्या इस बढ़ती हुई उम्र में एक बार फिर उम्मीदवार बनना चाहिए? चार बरस के मौजूदा कार्यकाल में बाइडन की उम्र और उनकी सेहत कई बार अमरीका की फिक्र का सामान बन चुकी है। वे बहुत सी बातों को भूल जाते हैं, कई मौकों पर वे लडख़ड़ाते नजर आते हैं, और अभी जब भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के साथ उनकी एक बहस का जीवंत प्रसारण हो रहा था, उस वक्त वे स्टेज पर तकरीबन सोए हुए से थे, और ट्रंप के अंतहीन हमलों के मुकाबले बाइडन का हाल इतना खराब था कि अब सुनने में आ रहा है कि उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी को चंदा देने वाले लोग उनको मनाने में लग गए हैं कि वे चुनाव न लड़ें। वैसे भी जितने किस्म के पोल अमरीका में हुए हैं, उनमें बाइडन खासे पिछड़े हुए हैं, और इस ताजा बहस के प्रसारण के बाद माना जा रहा है कि उनके लिए इससे हुए नुकसान से उबरना मुमकिन नहीं होगा।
सवाल यह उठता है कि बहुत जिम्मेदारी का कोई ओहदा संभालने वाले लोग उम्र या फिटनेस के किसी पैमाने पर कितने खरे उतरने चाहिए? कहने के लिए तो डोनल्ड ट्रंप भी 78 बरस के हैं, और बाइडन 81 बरस के। दोनों की उम्र में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन ट्रंप बेहतर सेहत में दिखते हैं, और अभी तक वे औरतों को दबोचने के तरीके बताते हुए दर्ज होते रहते हैं, और उनका हमलावर मिजाज अपने ओछे औजारों के साथ और कम उम्र का लगता है। दूसरी तरफ बाइडन की उम्र और सेहत दोनों को मिलाकर देखें, तो लगता है कि अभी तो राष्ट्रपति चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं, तब तक उनकी सेहत और कमजोर हो सकती है, और अगर वे जीतते हैं तो राष्ट्रपति का चार बरस का अगला कार्यकाल पार होने तक तो वे खासे बूढ़े हो चुके रहेंगे। आज की दुनिया में अमरीका को जितनी जायज और नाजायज दखल रखनी पड़ती है, क्या वह सब बाइडन के लिए बढ़ती उम्र और गिरती सेहत के साथ मुमकिन हो सकेगा?
लेकिन इस बारे में अमरीका के स्वास्थ्य विशेषज्ञों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों से बात करें तो यह समझ पड़ता है कि ट्रंप की तरह सांड जैसी ताकत से काम चाहे बाइडन न कर सके, लेकिन वे जितने बरसों से अमरीकी राजनीति में हैं उससे उन्हें एक अनोखा तजुर्बा हासिल है, और 1972 से अमरीकी संसद में पहुंचकर उन्होंने आधी सदी से अधिक देश और दुनिया को संसद और सरकार के भीतर से जिस तरह देखा है, वैसा तजुर्बा किसी सांड सरीखी सेहत वाले नेता को भी नहीं हो सकता। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बाइडन का यह असाधारण लंबा अनुभव उन्हें शारीरिक कमजोरी के बावजूद राष्ट्रपति पद का शानदार दावेदार बनाता है। मजबूत सेहत तो हर नौजवान या बुजुर्ग को हासिल हो सकती है, लेकिन आधी सदी का संसदीय तजुर्बा भला कितनों को हासिल हो सकता है, शायद किसी और को नहीं।
लेकिन इन खूबियों के बावजूद जो बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत से लोग सार्वजनिक रूप से उन्हें सुझा रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव लडऩे के अपने फैसले पर उन्हें फिर से विचार करना चाहिए। बाइडन ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि पिछले हफ्ते ट्रंप से बहस के दौरान वे बहुत बुरे जुकाम के शिकार थे, और उसकी वजह से थके हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर ही नीचे आकर कहे कि वे इस मुकाबले से बाहर निकल जाएं, तो ही वे पीछे हटेंगे। ट्रंप के तमाम उकसावे के बावजूद वे लगातार अपना काबू कायम रखे हुए हैं, और अपनी जीत को लेकर भरोसेमंद हैं।
ट्रंप की शक्ल में दुनिया के इस सबसे ताकतवर और असरदार मुल्क से उठ रहे सवाल दुनिया में कई और जगहों पर भी लोगों को परेशान कर सकते हैं, जहां 80 बरस के बुजुर्ग सत्ता की घोड़ी चढऩे के लिए दूल्हे बनकर तैयार खड़े हों। हिन्दुस्तान में कम से कम भाजपा में एक बात को बार-बार कहा गया है कि 75 बरस उम्र होने पर नेताओं को सत्ता से परे हो जाना चाहिए, हालांकि इस तर्क का इस्तेमाल अडवानी, मुरली मनोहर जोशी को किनारे करने के लिए किया गया, लेकिन कर्नाटक में येदियुरप्पा को 75 बरस का हो जाने के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। इसलिए ऐसा लगता है कि भाजपा में भी 75 बरस की सीमा को कुछ लोगों को किनारे करने की सहूलियत के लिए इस्तेमाल किया गया है।
उम्र और सेहत हर किसी की एक सरीखी नहीं रहती, इसलिए कई लोग जवान होते हुए भी मेहनत से दूर रह सकते हैं, और कई बुजुर्ग उम्र के लोग भी उनसे अधिक काम कर सकते हंै। अमरीका में एक संवैधानिक इंतजाम किया गया है कि अगर राष्ट्रपति ओहदे पर रहते हुए गुजर जाते हैं तो उपराष्ट्रपति को तुरंत ही राष्ट्रपति बना दिया जाता है। अगर जो बाइडन के सामने ऐसी कोई नौबत आती है, या फिर वे सेहत की किसी वजह से कोमा में चले जाते हैं, तो भी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जाता है, तो कमला हैरिस या कोई और उपराष्ट्रपति अमरीका को हमेशा ही मुसीबत में हासिल रहेंगे।
इसलिए ट्रंप जैसे बदचलन, अहंकारी, अनैतिक, सनकी, और भ्रष्ट व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने देने से बेहतर यही होगा कि उसके मुकाबले डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन, या किसी भी दूसरे उम्मीदवार को चुना जाए। जो बाइडन का जितना लंबा तजुर्बा है, और उन्होंने अमरीका को जिस तरह से एक बेहतर अर्थव्यवस्था मुहैया कराई है, जिस तरह डेढ़ करोड़ नौकरियां पैदा की हैं, 50 लाख अमरीकियों का पढ़ाई का लोन खत्म कर दिया है, वह असाधारण उपलब्धियां हैं। ट्रंप ने अपने चार साल के कार्यकाल में सिवाय नंगई के और कुछ नहीं किया था। इसलिए जो बाइडन उम्मीदवार बनने लायक हैं, और यह डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर की बात है कि वह किसे अपना उम्मीदवार बनाती है।
अगली चौथाई सदी में, 2050 तक हिन्दुस्तानियों की औसत उम्र 70 बरस से बढक़र 77 बरस पहुंच जाएगी, और एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय मेडिकल अध्ययन के मुकाबले हिन्दुस्तानियों में पुरूषों के मुकाबले महिलाओं की उम्र कुछ अधिक ही बढ़ेगी जो कि 75 बरस के आदमी के मुकाबले 80 बरस की हिन्दुस्तानी औरत की रहेगी। एक प्रमुख वैज्ञानिक पत्रिका, द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन के मुकाबले योरप के बहुत से देशों में 2050 तक लोग साढ़े 85 बरस औसत उम्र के हो सकते हैं, और इसकी एक वजह उनका बेहतर और समझदारी का खानपान है, और दूसरी वजह पैदल चलना, या साइकिल चलाना है जो कि योरप में बहुत अधिक प्रचलित है।
अब हिन्दुस्तान तो एक गाने पर अधिक भरोसा करता है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हों पचास हजार..., अब ऐसी कामना के बाद बहुत अधिक मेहनत करने की किसी को जरूरत नहीं रहती है, इसलिए हिन्दुस्तान के अधिकतर समाजों में खानपान लोगों की आर्थिक क्षमता के अनुपात में खासा गरिष्ठ रहता है। यहां तक कि जो धार्मिक उपवास होते हैं, उनमें भी खानपान बहुत ही भयानक दर्जे का रहता है जिससे सेहत का नुकसान छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। फिर संपन्नता बढऩे के साथ-साथ हिन्दुस्तान के अधिकतर लोग अपने घर के आसपास तक जाने के लिए भी कार या स्कूटर, मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, ताकि बदन पर किसी तरह का जोर न पड़े। कसरत और खेलकूद की फैशन भी गिने-चुने लोगों के बीच रहती है। इन्हीं सब वजहों से हिन्दुस्तानियों की औसत उम्र योरप की अधिकतम औसत उम्र से 8-10 बरस पीछे रहने जा रही है।
लेकिन औसत उम्र का बढ़ जाना, लोगों का अधिक समय तक जिंदा रहना, यह एक-दूसरे को शुभकामना देने की हद तक तो ठीक है कि लोग शतायु हों। लेकिन शुभकामना से परे शतायु होने वाले लोगों की जिंदगी का आखिरी एक चौथाई हिस्सा कैसा गुजरेगा, इसकी कल्पना भी भयानक है। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उन्हें भी 75 बरस की उम्र के बाद खराब हालत में ही देखा जाता है। शायद पूरी उम्र में वे सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, और बदन आखिरी के बरसों में पूरा हिसाब चुकता करता है। महंगे और बड़े अस्पतालों तक जिनकी पहुंच है, वे भी बुढ़ापा तकलीफदेह ही झेलते हैं। इसलिए आज जब दुनिया बढ़ती हुई औसत उम्र की भविष्यवाणी को लोगों की बेहतरी का एक पैमाना मानती है तो मुझे उसमें यह भी लगता है कि क्या यह बढ़ी हुई औसत उम्र, यानी आखिरी का बढ़ा हुआ हिस्सा पूरा का पूरा अधिक तकलीफ वाला हिस्सा नहीं रह जाएगा?
अभी इसी हफ्ते छत्तीसगढ़ में ही एक दिन में दो जगहों पर दो जवान बेटों ने अपने-अपने बाप निपटा दिए। अब ऐसा कत्ल होने पर तो इसकी खबर बनी, और हमारी नजर पड़ी, लेकिन खबर बनने के पहले तक परिवारों के भीतर जो तनाव रहता है, और जो खासकर घर के बूढ़ों के साथ चलता है, क्या वह सचमुच ही लंबा जीने लायक जिंदगी रहेगी? कुछ श्रवण कुमार किस्म के लोग भी होंगे जिन्हें यह चर्चा काफी कड़वी लगेगी कि हर घर में तो परिवार के बुजुर्गों का अपमान होता नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि अपमान से नीचे का दर्जा भी उपेक्षा का होता है जो चलने-फिरने में मजबूर बुजुर्गों को आहत करते रहता है। ऐसे में हिन्दुस्तान हो या योरप, जहां कहीं भी लोगों की औसत उम्र बढ़ेगी, और उसके चलते बुढ़ापा और लंबा हो जाएगा, वहां पर उन बुजुर्गों के साथ कई किस्म की भावनात्मक समस्याएं भी होंगी। आज भी बहुत से बुजुर्ग वृद्धाश्रमों को आल-औलाद के घर से बेहतर पाते हैं, क्योंकि वहां न तो किसी से उनकी कोई अपेक्षा रहती, और न ही कोई उपेक्षा उन्हें चोट पहुंचाती जो कि आल-औलाद के हाथों तकलीफ की बात रहती है।
इंसान अमर बनने की हसरत रखते हैं, दुनिया के तानाशाह, बड़े-बड़े नेता, बड़े कारोबारी, भला कौन ऐसे नहीं हैं जो कि मरना ही नहीं चाहते। कई लोगों के बारे में ऐसी कहानियां प्रचलन में रहती हैं वे कौन-कौन से इलाज कराकर, नौजवान लोगों का खून लेकर, खानपान में कुछ चुनिंदा और बहुत महंगी चीजें जुटाकर जिंदगी को जारी रखना चाहते हैं। सावधानी एक अच्छी बात है, और रोजाना के कामकाज से या कसतर से बदन को चुस्त-दुरूस्त रखना भी बड़ी अच्छी बात है क्योंकि उससे उम्र लंबी हो या न हो, जब तक जिंदगी है तब तक बदन फिट बने रहता है। सावधान लोग ये तमाम कोशिशें भी करते हैं, लेकिन इससे परे एक सबसे बड़ी वजह जिंदगी को लंबा और बेहतर बनाने में काम आती है, वह है लोगों का तनावमुक्त रहना।
यह बात कहना अधिक आसान है, इस पर अमल मुश्किल रहता है। आज जब हम अपने आसपास परिवारों के भीतर इतना तनाव देख रहे हैं कि लोग एक-दूसरे को मार डाल रहे हैं, या जरा-जरा सी बात पर जान दे दे रहे हैं, तो फिर यह बात बड़ी जाहिर है कि ऐसे परिवारों में तनावमुक्त रहना मुमकिन नहीं है, और तनाव के साथ लंबा जीना मुमकिन नहीं है। फिर एक बात यह भी है कि जिंदगी में अगर इतना तनाव है, तो उसे ढोते हुए इतना लंबा सफर करने का भी क्या फायदा?
फिलहाल आज इस मुद्दे पर मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि लोगों की हसरत बनी हुई है, वे मरते हुए भी एक और पीढ़ी देखकर जाना चाहते हैं, एक और पीढ़ी की शादी देखकर जाना चाहते हैं। ऐसी उम्मीदें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनके साथ-साथ लोगों को सेहतमंद और तनावमुक्त भी बने रहना होगा, तभी उनकी हसरतें मुमकिन हो पाएंगी। भारत की आबादी को लेकर 77.5 बरस की औसत उम्र एक नजरिए से देखने पर दहशत भी पैदा करती है, खासकर महिला को देखकर कि अगर उसकी औसत उम्र 80 बरस तक पहुंच जाएगी, और परिवार-समाज में उसकी आज जैसी दुर्गति बनी रहेगी, तो फिर वह उतना लंबा जीकर भी क्या करेगी?
इस कॉलम को पढऩे वाले अधिकतर लोगों के पास अपने-अपने परिवार की वजहें हैं, उनकी कहानियां हैं, और पिछली पीढ़ी के बुजुर्गों का भोगा हुआ सुख और दुख भी है। आज लोगों को यह सोचना चाहिए कि 2050 तक अगर औसत उम्र खासी बढऩे वाली है, तो क्या उसके लिए लोग तैयार हो रहे हैं, तन और मन को, और धन को भी तैयार रख रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर परिवार के भीतर सोचने की जरूरत है, और हो सकता है कि आज सोची गई बात का ऐसा असर हो कि जिंदगी के आखिरी के बढ़े हुए बरस जीना कुछ आसानदेह और सुखभरा हो जाए।
मेरे करीब के एक कस्बे की खबर है कि एक आदमी ने देर रात अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। 75 बरस के पति ने 72 साल की पत्नी से देर रात सेक्स की फरमाईश की, पत्नी ने मना कर दिया, तो उसने फावड़े से कई वार करके पत्नी को वहीं मार डाला। गिरफ्तार पति से ही यह बात पुलिस को पता लगी। 75 और 72 बरस की उम्र में सेक्स को लेकर अलग-अलग दर्जे की जरूरतें रहने की बात तो बिल्कुल नई सरीखी है, लेकिन काफी कम उम्र में ही अधेड़ हो जाने पर ही भारत में बहुत से जोड़ों के बीच यह दिक्कत होने लगती है। अधिक जगहों से यह सुनाई पड़ता है कि पत्नी की दिलचस्पी सेक्स में पहले खत्म हो गई है, और पति की जरूरत बाकी है, और इसलिए वह बाहर मुंह मारने लगा है। जितने जोड़े, उतने किस्म की बातें।
अब अगर जमीनी हकीकत को देखें तो भारत में परिवारों का ढांचा, समाज की सोच, और धर्म का प्रभाव, इन सबका नतीजा यह होता है कि शादीशुदा जोड़ों के बीच भी देहसंबंध की गुंजाइश या तो घटने लगती है, या फिर जोड़ों के बीच के तनाव ऐसे रहते हैं कि मन तन को पास आने नहीं देता। आम हिन्दुस्तानी आदमी इतने किस्म की थकान लेकर, या मानसिक तनाव लेकर बिस्तर पर पहुंचते हैं कि वहां बीवी के साथ अधिक कुछ होने या करने की गुंजाइश नहीं रहती है। दूसरी तरफ घर के काम के बोझ से लदी हुई, अब घर-घर में बन गए शौचालयों के लिए मीलों से पानी ढोकर लाने वाले टूटते हुए बदन वाली औरत को बिस्तर पर नींद और आराम से जरूरी और कुछ नहीं लगता। इसलिए बहुत से जोड़े ऐसे हैं जो एक ही कमरे में परिवार के और लोगों के साथ रहने की मजबूरी के चलते, या बगल के कमरे तक आवाज जाने की आशंका में जीते हुए किसी सेक्स के लायक बचते भी नहीं हैं।
भारत के संयुक्त परिवारों में घर की महिला से बिल्कुल सुबह से लेकर देर रात तक लगातार काम की उम्मीद की जाती है, और उससे कुछ पाने वालों की लिस्ट में उसके पति का नाम सबसे आखिर में रहता है। परिवार के बाकी बच्चे-बूढ़े, जवान या अधेड़ जोड़े की जरूरत को समझ भी नहीं पाते, या समझना ही नहीं चाहते। नतीजा यह होता है कि संयुक्त परिवार बहू की गोद तो हमेशा भरी देखना चाहता है, लेकिन बहू को उसके पति संग अलग से समय मिल सके, इसमें उसकी खास दिलचस्पी नहीं रहती।
अब इतनी बातों के बाद धर्म का दखल शुरू होता है, जो कि सामान्य और स्वाभाविक शारीरिक जरूरतों वाले जोड़ों में भी सेक्स के खिलाफ एक नापसंदगी पैदा करते रहता है। देह की जरूरतों को काम-वासना जैसे अपमानजनक नाम दिए जाते हैं, और लोगों के दिमाग में लगातार यह भरा जाता है कि उन्हें सेक्स जैसी चीज में नहीं उलझना चाहिए, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए जिससे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। अब अगर स्वर्ग में भी सेक्स से ऐसा ही परहेज सिखाया जाएगा, तो बिना सेक्स वाली वह जगह भला कैसे स्वर्ग कही जा सकेगी? धर्म से जुड़े हुए भारत के एक आध्यात्मिक कहे जाने वाले संगठन की तो नसीहत यही है कि पति-पत्नी को भाई-बहन की तरह रहना चाहिए। अब अगर वे भाई-बहन की तरह रहेंगे, तो देहसंबंध किससे बनाएंगे? अगर जीवनसाथी को ही भाई-बहन मानना है, तो फिर देह की जरूरत के लिए चारों तरफ अनैतिक कहे जाने वाले काम करने होंगे। लेकिन धर्म और आध्यात्म लोगों को स्वाभाविक सेक्स से दूर धकेलते रहते हैं, फिर चाहे देश के एक सबसे बड़े प्रवचनकर्ता और स्वघोषित संत आसाराम अपनी सेक्स की जरूरतों के लिए नाबालिग से बलात्कार ही क्यों न करता रहे। हिन्दुस्तान के जो लोग धर्म और आध्यात्म के अधिक झांसे में रहते हैं, उनका सेक्स-जीवन बर्बाद होने का बड़ा खतरा मंडराते रहता है।
धर्म और समाज, परिवार और पारंपरिक सामाजिक शिक्षा के चलते हुए भारत के लोगों में सेक्स को लेकर हिचक और झिझक भर जाती है। नतीजा यह होता है कि जोडिय़ों में से किसी एक की जरूरत पूरी नहीं होती, दूसरे को परवाह नहीं रह जाती। ऐसे में विवाहेत्तर संबंध बनने लगते हैं, और कई जगहों पर आगे जाकर प्रेमिका की हत्या, या प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या जैसी बातें होने लगती हैं। जोड़ों के बीच की हिंसा लगातार बढ़ती चल रही है, इसकी एक वजह भारतीय समाज में सेक्स की जरूरत को कम आंकना है, और लोगों को धर्म की तरफ धकेलना है। इससे लोग भी इस झांसे में आ जाते हैं कि दो-दो बच्चे हो जाने के बाद सेक्स की क्या जरूरत है। जबकि यह पूरी तरह धर्मान्ध सोच है कि मनचाही संख्या में बच्चे हो जाने के बाद लोगों को मन भजन-पूजन में लगाना चाहिए। कई परिवारों में जीवनसाथियों के बीच इस बात को लेकर झड़प भी रहती है कि क्या अब इन बातों की उम्र रह गई है? धर्म सेक्स को लेकर लोगों के मन में एक बड़ा अपराधबोध पैदा कर देता है कि बच्चे हो जाने के बाद भी उनका मन इसी काम-वासना में लगा हुआ है।
ऑस्ट्रेलिया और अमरीका के एक सबसे बड़े मीडिया कारोबारी रूपर्ट मर्डोक ने अभी 93 बरस की उम्र में 5वीं शादी की है, और इस बार यह शादी 67 बरस की एक रूसी मालिक्यूलर बायोलॉजिस्ट से हुई है। लोगों की तन और मन की जरूरत कब तक जारी रहती है, इसके लिए कोई एक पैमाना बनाना जायज नहीं है। लोगों को धर्म और समाज, आध्यात्म और परिवार की नसीहतों से परे अपनी शादीशुदा जिंदगी की जरूरतों पर खुद फैसले लेना चाहिए।
छत्तीसगढ़ में 46 डिग्री तापमान पर एक धार्मिक प्रवचन चल रहा है, और कुछ दिन पहले इसकी तैयारी में हजारों महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर नंगे पैर शोभायात्रा भी निकाली थी। अभी भी जिस जगह यह प्रवचन चल रहा है, वहां लाखों लोगों की आवाजाही है, और कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम रहता है। सत्तारूढ़ भाजपा के एक नेता ने कल ही ट्विटर पर यह लिखा है कि इतनी गर्मी में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में 8 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया। स्थानीय नागरिकों का दावा है कि अब तक 6 मौतें हो चुकी हैं। तत्काल इस आयोजन पर रोक लगे, प्रशासन इस पर ध्यान दें। और लोगों ने भी इस पर लिखा है कि कथावाचकों को अप्रैल, मई, और जून के महीनों में कार्यक्रम नहीं रखने चाहिए। किसी ने लिखा है कि इस महाराज को खुद ही यह कार्यक्रम रखना नहीं था, या अब बंद कर देना चाहिए, किसी के कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक और ने लिखा है कि महाराज को पैसा कमाने से फुर्सत मिले, तो आम नागरिकों की सोचें। इतनी गर्मी में कोई ऐसा आयोजन करता है, जबकि गर्मी का रेड अलर्ट जारी हुआ है। एक व्यक्ति ने तंज कसते हुए कहा है कि दो सौ बेलपत्र चढ़ाने बोलिए, ठीक हो जाएगा। किसी और ने याद दिलाया है कि इसी प्रवचनकर्ता के मध्यप्रदेश में भी रूद्राक्ष वितरण के दौरान बहुत से मौतें देखने मिली थी। कुछ लोगों ने यह याद दिलाया है कि लोगों को अपने घर से ही कथा सुननी चाहिए। एक ने ट्वीट करने वाले भाजपा नेता को याद दिलाया कि इतनी भरी गर्मी में यह जानलेवा आयोजन करने की अनुमति भाजपा सरकार ने ही दी है। एक ने लिखा है कि चलिए बहुत जल्द जाग गए, फिलहाल कथा समाप्त हो चुकी है। एक ने सवाल उठाया है कि 6 मौतों की जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। एक व्यक्ति ने लिखा है कि महाराज को होश नहीं है क्या, इसी भीषण गर्मी में अपने प्रवचन रद्द करना चाहिए, मरने वालों को दस-दस लाख मुआवजा देना चाहिए।
अभी कल की ही एक खबर थी कि डेढ़ बरस पहले राजस्थान से निकले पति-पत्नी 665 किलोमीटर की दंडवत यात्रा करके उज्जैन पहुंचे हैं। इसका वीडियो देखना भी भयानक था जब चारों तरफ तपती सडक़ पर नंगे पैर यह बुजुर्ग जोड़ा चल रहा है, और ये सडक़ों पर लेट-लेटकर आगे बढ़ रहे हैं। 55 बरस उम्र का आदमी एक दिन में करीब डेढ़ किलोमीटर की यात्रा इस तरह कदम-कदम पर दंडवत लेटकर इंच-इंच आगे बढ़ते दिखता है, और पत्नी भी झोले में थोड़ा सा सामान लेकर साथ चल रही है। रास्ते में कभी वे कुछ खरीदकर खा लेते हैं, कभी लोग कुछ खिला देते हैं। अब आज जब सरकार लोगों को गर्मी में घर से बाहर न निकलने की सलाह दे रही है, देश भर में सैकड़ों लोग एक-एक दिन में लू से मर रहे हैं, तब यह बुजुर्ग जोड़ा डेढ़ साल के इस कठिन, तकलीफदेह, और जानलेवा तीर्थयात्रा पर है। नवतपा के बीच सफर इसी तरह जारी है।
आस्था लोगों की तर्कशक्ति को पूरी तरह खत्म कर देती है। अब इस जोड़े ने डेढ़ बरस का वक्त ऐसी यात्रा पर लगा दिया है, जिससे उनकी निजी आस्था जरूर पूरी हो रही है, कोई मन्नत भी पूरी हो रही है, लेकिन इससे समाज का भला क्या भला हो रहा है? और जहां तक ईश्वर की बात है, तो पत्थर की प्रतिमाओं, लकड़ी के सलीब, या अमूर्त ईश्वरों, धार्मिक ग्रंथों की उपासना और आराधना से किसी ईश्वर का भला होते तो किसी ने देखा नहीं है। बहुत से लोग तरह-तरह के कठिन इरादे तय कर लेते हैं, और फिर बरसों तक उसे पूरा करने में लगे रहते हैं। अगर सचमुच ही कहीं कोई ईश्वर है, तो उसे क्यों ऐसी बातों को बढ़ावा देना चाहिए? अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपने पास ही एक व्यक्ति को अपनी जीभ काटकर किसी देवता को चढ़ाते हुए देखा है, और कहीं पर किसी देवता को खुश करने के लिए एक इंसान ने अपने चार बरस के बेटे की बलि दे दी। भला कौन सा ऐसा ईश्वर हो सकता है जो एक नन्हें बच्चे की बलि पाकर खुश हो, और अगर सचमुच ही ऐसा कोई ईश्वर है, तो वह पूजा-उपासना के लायक तो हो भी नहीं सकता।
इस तरह के अंधविश्वासी आस्थावान लोगों को वह मिसाल दिखाने की जरूरत है जिसमें किसी एक व्यक्ति ने पहाड़ पर से आने-जाने का रास्ता बनाना तय किया, और कई बरस हर दिन खुदाई करके उसने अकेले सडक़ ही बना दी। कई ऐसे लोगों की असल जिंदगी की कहानियां सामने है जिन्होंने किसी बंजर पहाड़ पर पौधे लगाने शुरू किए, और आज 25-30 बरस बाद उस रूखे-सूखे पहाड़ की एक-एक इंच जमीन हरियाली से पट गई है। अकेले अपने दम पर अभियान छेडऩे वाले बहुत से लोग हैं, मुम्बई में एक विख्यात कार्टूनिस्ट आबिद सुरती हैं जो किसी प्लंबर को लेकर घर-घर जाकर दरवाजा खटखटाते हैं, और पूछते हैं कि उनके घर कोई नल तो नहीं टपकता? अपने पैसों पर अपनी मेहनत से कभी प्लंबर ले जाकर, तो कभी खुद औजार चलाकर वे पानी की बर्बादी वाली टोटियों को सुधारने का अभियान चला रहे हैं, और पूरी तरह अकेले चला रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं जो जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदाता जुटाने का काम करते हैं, और हमारे आसपास ही ऐसे कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपना भी खून दिया, और दूसरे दानदाता भी जुटाए।
हमारा ख्याल है कि मन्नत तो किसी भी तरह की मानी जाती है, और लोगों की यह निजी आजादी है। लेकिन अगर इस मन्नत का धरती पर कोई इस्तेमाल भी हो, तो भी वह काम की हो सकती है। डेढ़ बरस का वक्त सिर्फ तकलीफ पाकर एक सफर में गुजार देना, इससे न तो उज्जैन के महाकाल को कुछ हासिल होना है, न ही समाज को इससे कोई फायदा हुआ। इसके बजाय यह जोड़ा अगर 665 दिन अपने शहर के अस्पताल जाकर रोज 8-10 घंटे मरीजों की मदद करता, कहीं व्हीलचेयर धकेलता, कहीं मरीजों के स्ट्रेचर ले जाने में मदद करता, तो उससे समाज का भी भला होता। अलग-अलग बहुत से धर्मों के लोग महीने में या हफ्ते में एक दिन कई घंटे उपासना-आराधना में गुजारते हैं, अगर उन्हें अपने ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया में लोगों के दुख-तकलीफ को दूर करने की बात सूझती, तो उससे उनका ईश्वर भी, अगर कहीं होता तो, खुश हो सकता था। किसी दिन कुछ खाना नहीं, किसी दिन कुछ पीना नहीं, किसी दिन किसी रंग के कपड़े पहनना, किसी दिन उपासना स्थल जाना, इससे किसी को क्या हासिल होता है? यह अपने आपको बेवकूफ बनाने के तरीके रहते हैं। अगर सचमुच ही लोगों को लगता है कि दुनिया उनके ईश्वर की बनाई हुई है, तो उन्हें इस दुनिया के जरूरतमंद लोगों की सेवा करना चाहिए, धरती की बर्बादी रोकना चाहिए। मजे की बात यह है कि कोई भी धर्मगुरू लोगों को ऐसा रास्ता सुझाते नहीं दिखते। भला अपनी दुकान बंद करवाना कौन चाहेंगे? यह तो कुछ वैसा ही होगा कि फास्ट फूड बेचने वाले लोग यह पर्चा छपवाकर आने वालों को थमाते रहें कि फास्ट फूड से सेहत का कितना नुकसान होता है। अब अगर प्रवचनकर्ता या मुल्ला, पुजारी, और पादरी लोगों को ईश्वर की आराधना के लिए कचरा साफ करने, गरीबों की मदद करने, अस्पताल जाकर काम करने की नसीहत देंगे, तो खुद का धंधा बंद ही हो जाएगा। इसलिए धर्म प्रायश्चित, दान, और पाप-मुक्ति के बड़े कामयाब फॉर्मूले पर काम करता है जो कि हिट हिन्दी फिल्में बनाने के फॉर्मूलों सरीखा है। इसलिए ऐसे धर्म को 665 किलोमीटर की दंडवत तीर्थयात्रा को बढ़ावा देना ठीक लगता है, बजाय इतने दिनों के किसी सार्थक उपयोग के।
ब्रिटिश सरकार ने स्कूली बच्चों को यौन शिक्षा देने की मौजूदा नीति को बदलते हुए 9 बरस उम्र तक के बच्चों को किसी भी तरह की यौन शिक्षा देने पर रोक लगा दी है। सरकार की नीति के बारे में ब्रिटिश मीडिया में बड़ी बहस छिड़ी हुई है, और अब तक स्कूलों में यह शिक्षा देने वाले शिक्षक इस नई सीमा के खिलाफ हैं। इस नीति में बच्चों को सेक्स और रिश्तों के बारे में पढ़ाया जाता है, अब तक 9 बरस से छोटे बच्चों को भी काफी कुछ बताया जाता था, लेकिन सरकार अब इस पर रोक लगा रही है। शिक्षकों का मानना है कि बच्चों के मन में जिस उम्र से जिज्ञासा आने लगती है, उस उम्र से अगर उन्हें उनके जवाब नहीं मिलेंगे, तो फिर वे गलत जगहों से वे जवाब तलाशने लगेंगे जो कि पोर्नोग्राफी की वेबसाइटें भी हो सकती हैं, और इसके अलावा वे आसपास गलत लोगों के शिकार भी हो सकते हैं। ब्रिटिश शिक्षकों का यह मानना है कि चार बरस की उम्र से ही बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श की जानकारी समझाना शुरू हो जाना चाहिए ताकि वे अपने यौन शोषण से बच सकें। ऐसा न होने पर वे कुछ लोगों के नाजायज छूने का मतलब नहीं निकाल पाएंगे। इस शिक्षा के तहत स्कूली बच्चों को ट्रांसजेंडर और दूसरे एलजीबीटीक्यूआई समुदाय के लोगों के बारे में भी बताया जाता है, उनके अपने शरीर के बारे में बताया जाता है, और गर्भधारण जैसी चीजों को भी समझाया जाता है। ब्रिटेन कम उम्र में गर्भवती होने वाली स्कूली छात्राओं की समस्या भी झेल रहा है, और यह माना जाता है कि छात्राओं को यौन शिक्षा मिलने से वे गर्भवती होने से, या सेक्स-बीमारियों से बचेंगी।
ब्रिटिश अखबार गॉर्डियन के एक इंटरव्यू में ऐसी एक जानकार शिक्षा शास्त्री ने यह कहा कि अब बच्चों के तन, मन, और उनकी समझ, ये सब कुछ पहले के मुकाबले कम उम्र में विकसित हो रहे हैं। इसलिए उनके मन में जिज्ञासाएं कम उम्र में पैदा हो रही हैं। ब्रिटेन में अभी सत्तारूढ़ संकीर्णतावादी कंजरवेटिव पार्टी का शासन है जिसके कई सांसद इस बात को लेकर नाखुश हैं कि बच्चों को स्कूलों में कम उम्र से ही शरीर, सेक्स, और यौन संबंधों के बारे में जरूरत से अधिक पढ़ाया जा रहा है। एक किस्म से मौजूदा सरकार जो कि चुनाव की घोषणा कर चुकी है, और दो महीने की भी मेहमान नहीं है, वह एक बड़ा फैसला ले रही है जिससे वहां के सारे लोग सहमत भी नहीं हैं।
मैं ब्रिटेन के इस ताजा घटनाक्रम को हिन्दुस्तान के अपने इलाके से जोडक़र देखना चाहता हूं जहां पर हर दिन एक से अधिक पुलिस रिपोर्ट या गिरफ्तारी ऐसे मामले में हो रही है जिसमें नाबालिग को बहला-फुसलाकर किसी बालिग ने उससे सेक्स किया, ऐसा कहा जाता है कि शादी का झांसा दिया, और फिर शादी नहीं की तो इस सेक्स को बलात्कार कहकर उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत से ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को चाहे जो सजा हो जाए, यह बात समझने की जरूरत है कि ऐसे देहसंबंधों से, और बाद में मामले के अदालत तक पहुंचने से खुद लडक़ी का भी बड़ा नुकसान होता है। उसे नाबालिग रहते हुए ऐसे देहसंबंधों के तमाम खतरों से वाकिफ तो रहना चाहिए था।
आज देश भर में हर दिन कई जगहों पर नवजात शिशु नालों या घूरों पर फेंके हुए मिलते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ ऐसी कम उम्र नाबालिग लड़कियों के बच्चे भी हों जो कि भारत की क्रूर समाज व्यवस्था के चलते इन्हें जन्म देने का हौसला न कर पाती हों। अभी सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे मामले पहुंचे हुए जिनमें बलात्कार या किसी दूसरे तरह से गर्भवती हुई नाबालिग लडक़ी की ओर से मेडिकल समय सीमा पार हो जाने के बाद भी गर्भपात की इजाजत मांगी जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने अजन्मे बच्चे के अधिकार को अधिक बड़ा मानते हुए 7वेें-8वें महीने के ऐसे बच्चे के गर्भपात की इजाजत नहीं दी। अब नाबालिग बच्चे हिन्दुस्तान में जगह-जगह दूसरे नाबालिगों से बलात्कार करते पकड़ा रहे हैं, लड़कियां जगह-जगह गर्भवती हो रही हैं, और सेक्स से फैलने वाली बीमारियों के तो कोई पुलिस-आंकड़े होते नहीं हैं। इसलिए अपने बदन, सेक्स, और रिश्तों की जो पढ़ाई ब्रिटेन में होती है, और जिसकी उम्र अब बढ़ाकर 9 बरस की जा रही है, वैसी कोई पढ़ाई हिन्दुस्तान में किशोरावस्था में पहुंचने पर भी नहीं होती। नतीजा यह होता है कि लडक़े-लड़कियां मां-बाप बनने के लिए शारीरिक रूप से तैयार हो जाते हैं, सेक्स उनकी एक स्वाभाविक जरूरत बन जाता है, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी जरा भी नहीं रहती। नतीजा यह होता है बहुत से लोग असुरक्षित सेक्स में फंस जाते हैं, बहुत से नाबालिग सेक्स-वीडियो में फंस जाते हैं, और फिर ब्लैकमेलिंग से लेकर तमाम दूसरे किस्म के जुर्म के शिकार हो जाते हैं।
ऐसी हालत रहने पर भी हिन्दुस्तान में आज बच्चों और किशोरों को, छात्र-छात्राओं को, किसी को भी देह की शिक्षा देने पर समाज का एक दकियानूसी तबका झंडे-डंडे लेकर उठ खड़ा होता है। यह तबका हिन्दुस्तान की एक इतिहास में कभी न रही हुई ऐसी संस्कृति का हवाला देता है जिसमें मानो सेक्स रहा ही न हो। इनके तेवरों का नतीजा यह होता है कि नई पीढ़ी के बदन सेक्स के लायक हो जाते हैं, वे सेक्स में उलझ जाते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में कोई वैज्ञानिक और सामाजिक समझ नहीं दी जाती। जिन नाबालिग बच्चों को सेक्स में नहीं उलझना चाहिए था, उनके सामने भी सीखने का अकेला जरिया पोर्नोग्राफी रह जाता है, आसपास के ऐसे मुजरिम रह जाते हैं जिनकी कि बच्चों से सेक्स में दिलचस्पी रहती है, आसपास के अपने से उम्र में कुछ बड़े लोग रह जाते हैं जो कि आसानी से बरगलाकर अपने से छोटे लोगों को सेक्स की तरफ धकेल देते हैं या खींच लेते हैं।
किसी भी देश या समाज को पाखंड में जीना छोड़ देना चाहिए। लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि आज की पीढ़ी कौन से युग में जी रही है, उस पर कौन से प्रभाव हैं, प्रकृति ने नई पीढ़ी के बदन में किस उम्र से कैसी जरूरतें पैदा करना शुरू कर दिया है। इसके साथ-साथ आज इंटरनेट की मेहरबानी से पूरी दुनिया एक गांव की तरह होकर रह गई है, और सोशल मीडिया के तरह-तरह के प्लेटफॉर्म तमाम बच्चों को बाकी दुनिया से रूबरू करवा देते हैं। नतीजा यह होता है कि एक देश के टीनएजर्स दूसरे देश के किशोर-किशोरियों के सामने सांस्कृतिक चुनौतियां पेश करते हैं, और कहीं जवाबी रील बनने लगती हैं, तो कहीं जवाबी टिकटॉक।
ऐसे में बच्चों को उनके बदन और दूसरे के साथ संबंधों की बुनियादी शिक्षा से बचाकर इस पीढ़ी को एक खतरे के अलावा और कुछ नहीं दिया जा रहा। बच्चों के तन और मन तो अपने वक्त पर जवान हो जाएंगे, लेकिन तब तक उनकी समझ अगर समाज की कोशिश से अनजान बनाकर रखी जाएगी, तो वे बदन और रिश्तों के खतरों को भी नहीं समझ पाएंगे, और हिन्दुस्तान में आज यह बात बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान कर रही है।
दकियानूसी राजनीतिक विचारधारा को जहां मौका लगता है, वह समाज से प्रगतिशील समझ की चीजों को पीछे धकेलने लगती है। ब्रिटिश सरकार की इस ताजा नीति की जमकर आलोचना भी हो रही है, और यह बात भी साफ है आज वहां जिस उम्र के बच्चों को इस शिक्षा की जरूरत है, उससे कम से कम 50 बरस अधिक बड़े सांसद अपनी सरकार पर दबाव डालकर यौन शिक्षा को 9 बरस की उम्र तक रोक रहे हैं। यह बात तय है कि आधी सदी पहले की तन-मन की सामाजिक जरूरतें अलग थीं, आज कम्प्यूटर-मोबाइल, और सोशल मीडिया के युग में ये जरूरतें एक अलग ही दर्जे की हो गई हैं। राजनेता हर मामले में फैसले लेने के लिए सबसे काबिल नहीं रहते हैं। खासकर शिक्षा नीति से तो नेताओं को अपने आपको दूर रखना चाहिए क्योंकि यह सिर्फ विशेषज्ञों की समझ की बात है, और उन्हीं के फैसलों पर इन्हें छोडऩा चाहिए। राजनेताओं को जिंदगी के हर दायरे के विशेषज्ञ मान लेने से ऐसे तमाम दायरों का कुछ या काफी हद तक नुकसान होगा, उससे बचना चाहिए, और आने वाली पीढ़ी को समझदार और सावधान बनने से रोकना नहीं चाहिए।
अमरीका की समाचार पत्रिका, टाईम, ने वहां के कई शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों से बात कर यह नतीजा निकाला है कि वहां अल्पसंख्यक कहे जाने वाली नस्लों, रंगों, और राष्ट्रीयता की महिलाओं पर परिवार नियोजन के लिए दबाव अधिक रहता है। अमरीका में आबादी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, और वहां कागजों पर संवैधानिक अधिकार पूरी तरह बराबर हैं, लेकिन फिर भी जगह-जगह से नस्लीय भेदभाव की शिकायतें आती हैं, और काले लोग, या लैटिन, मैक्सिकन, दूसरे अश्वेत समुदाय भेदभाव अधिक झेलते हैं। योरप के एक देश ग्रीनलैंड के बर्फीले इलाके में रहने वाले एक समुदाय की आबादी बढऩे से रोकने के लिए दूर राजधानी से अफसरों ने यह तय किया था कि इस इलाके की छोटी-छोटी स्कूली लड़कियों के बदन में भी गर्भनिरोधक फीट कर दिए जाएं। 1960 और 70 के दशक में एक समुदाय की आबादी को रोकने के लिए अफसरों और डॉक्टरों ने यह तय किया था, और छोटी-छोटी नाबालिग लड़कियों के मां-बाप की जानकारी के बिना, इन लड़कियों को कुछ समझाए बिना, उनके बदन में गर्भनिरोधक फीट कर दिए गए थे। अब बीते कुछ बरसों में जबसे इस शादी का भांडाफोड़ हुआ है, वहां की सरकार इस मामले की जांच करा रही है। दूनिया के कुछ और देशों में भी आदिवासी, मूलनिवासी, या दूसरे कमजोर तबकों के साथ ताकतवर, शहरी, शिक्षित तबके ऐसा ही करते आए हैं। अब अमरीका से आई यह खबर इसलिए कुछ चौंकाती है कि वहां की भाषा में जो लोग अल्पसंख्यक हैं, उनके खिलाफ अगर वहां की गोरी और ताकतवर आबादी इस तरह के भेदभाव की हिंसा करते आई है, तो वह अमरीका के अपने मानवाधिकार के दावों के खिलाफ जाने वाली बात है।
लेकिन जरा सी देर के लिए यह सोचें कि डॉक्टर तबका ऐसा करता क्यों होगा? क्या इसके पीछे डॉक्टरों की यह सामाजिक जागरूकता और जवाबदेही भी हो सकती है कि कैसे उनके पास आने वाली महिलाएं अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के बावजूद और बच्चे पैदा करने पर रोक नहीं लगा रही हैं? डॉक्टरों में हर कोई नस्लवादी या गैरजिम्मेदार हों ऐसा भी जरूरी नहीं है। दूसरी तरफ हर डॉक्टर को अपने देश के अल्पसंख्यक तबकों के साथ ऐसा बर्ताव करने से कोई फायदा होता हो यह भी जरूरी नहीं है। इसलिए हो सकता है कि कुछ डॉक्टर अपने मरीज के भले के लिए, उसके पारिवारिक और सामाजिक भले के लिए भी उसे गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करते हों। जिस अमरीका से यह शोध निष्कर्ष सामने आया है, उस अमरीका में भी यही तमाम तबके अधिक गरीबी के शिकार हैं। ऐसे में उन्हें कम बच्चे की सलाह देने के पीछे कोई डॉक्टरी विशेषज्ञता होना जरूरी नहीं रहता, सामान्य समझबूझ और सद्भावना से भी ऐसी सलाह दी जा सकती है।
अब हिन्दुस्तान में शाहरूख खान जैसे लोग सरोगेसी से तीसरा बच्चा पाते हैं, लेकिन उसे पालने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ किसी गरीब परिवार में तीसरे बच्चे उस परिवार पर बहुत बड़ा बोझ रहते हंै, तब तक जब तक कि वे पढ़-लिखकर या कोई हुनर सीखकर किसी काम-धंधे में न लग जाएं। लेकिन हिन्दुस्तान के आम मुस्लिम परिवार की गरीबी तीसरे बच्चे की वकालत नहीं कर सकती। और चूंकि देश में दलित, आदिवासी, मुस्लिम ऐसे तबके हैं जिनमें गरीबी अधिक है, तो यह बात जाहिर है कि ऐसे तबकों को परिवार नियोजन की, नसबंदी या गर्भनिरोधकों की जरूरत आर्थिक और सामाजिक कारणों से भी अधिक है। यह बात पूरे देश पर आबादी के बोझ से कहीं अधिक इन परिवारों के अपने बोझ से जुड़ी हुई अधिक है कि क्या ये सचमुच एक और बच्चे का खर्च उठा सकते हैं? क्या ये इतने बच्चों के खानपान, पढ़ाई-लिखाई, इलाज, और व्यक्तित्व विकास का खर्च ढो सकते हैं ?
अमरीका की पूरी शोध को देखे बिना हम इस बात को लिख रहे हैं, इसलिए इसे अमरीका के इस निष्कर्ष से जोडक़र न देखा जाए। इसे दुनिया के उन तमाम देशों पर लागू करके देखा जाए जहां पर गरीबी हैं, या जिस धर्म और जाति के लोग, रंग और नस्ल के लोग अधिक गरीब हैं, उनसे जोडक़र देखा जाए। हमारा ख्याल है कि डॉक्टर भी अपने मरीज के बदन के साथ-साथ उसकी पारिवारिक और सामाजिक स्थिति को भी देखते हैं। हम अपने आसपास ही ऐसे डॉक्टर देखते हैं जो मरीज की आर्थिक स्थिति देखते हुए कई बार कम दाम की दवाईयां लिखते हैं, कम खर्चीले इलाज बताते हैं। अब ऐसे गरीब मरीजों के धर्म और उनकी जाति को लेकर एक निष्कर्ष यह भी निकल सकता है कि वे दलित-आदिवासी, या धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन अगर उनकी फिक्र मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए तो है, जैन अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, तो इसकी एक वजह यह हो सकती है कि जैन समाज आमतौर पर संपन्न रहता है, उसे परिवार को छोटा रखने की नसीहत देना उतना जरूरी नहीं रहता, जितना कि एक गरीब परिवार को देना रहता है।
आज हिन्दुस्तान जैसे देश में कुछ लोग मुस्लिमों की आबादी बढऩे के आंकड़ों को लेकर एक भयानक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। आंकड़े अपने आपमें कुछ नहीं बोलते, उन्हें अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल करके उनसे कई तरह के मतलब निकाले जाते हैं। इनमें से एक भारत में मुस्लिम आबादी की दहशत पैदा करने का भी है। अब ऐसी किसी मुस्लिम-विरोधी नीयत के बिना भी अगर कोई आमतौर पर, अमूमन गरीब मुस्लिम समाज को कम बच्चों की सलाह दे, तो वह साम्प्रदायिक मानने के बजाय उस समुदाय के भले की सलाह मानना बेहतर होगा क्योंकि कम बच्चों का ख्याल मुस्लिम परिवार बेहतर तरीके से रख सकेंगे, उन्हें अधिक दूर तक आगे बढ़ा सकेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी का मुकाबला करने के लिए जो हिन्दू नेता हर हिन्दू परिवार को चार, छह, या दस तक बच्चे पैदा करने का फतवा देते हैं, वे हिन्दुओं के दुश्मन के अलावा और कुछ नहीं है क्योंकि आज बहुत संपन्न परिवार भी दस बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते, और आम परिवार में दस बच्चों का मतलब हर बच्चे का कुपोषण का शिकार होना, और अधिक से अधिक एक मजदूर बनने जितना काबिल बनना हो जाएगा।
जो लोग आबादी बढ़ाने की बात करते हैं, या बढ़ाते हैं, वो खुद अपना नुकसान सबसे अधिक करते हैं। अमरीका में भी जो समुदाय आज गोरों के मुकाबले गरीब हैं, उनमें अधिक बच्चे पैदा करने से उनका कुछ भला नहीं होता है। अब वहां के डॉक्टर अगर किसी साम्प्रदायिक आधार पर इन नस्लों की आबादी बढऩे देने के खिलाफ हैं, तो वह एक अलग जांच और कार्रवाई का मुद्दा है। हम इस खबर की बड़ी सीमित जानकारी के आधार पर आज सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जो तबके कमजोर हैं, उन्हें बहुत अधिक बच्चे पैदा करने के खिलाफ समझाना उन तबकों का नुकसान करना नहीं है, उनका फायदा करना ही है। अब ऐसे फायदे के साथ-साथ अगर कोई साम्प्रदायिक या नस्लभेदी नजरिया है, तो वह एक अलग बात है, लेकिन हम आमतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी समाज में बच्चों की सीमित संख्या के हिमायती हैं, और इसे उस समुदाय के खिलाफ साजिश मानना गलत होगा।
दुनिया में अगर अपनी ही खरीदी हुई किताबों से ज्ञान हासिल करना रहता, उन्हें पढऩा रहता, तो लोग बहुत जरा सा पढ़ पाते। सबसे गरीब से लेकर सबसे संपन्न देशों तक अधिकतर लोगों का किताब पढऩा लाइब्रेरी पर निर्भर करता है। सार्वजनिक लाइब्रेरी जैसे-जैसे घट रही हैं, वैसे-वैसे लोगों की पढऩे की आदत कम हो रही है। और अब तो दुनिया के कम सभ्य और कम समझदार देशों में लाइब्रेरी की जरूरत ही नहीं समझी जा रही है। फिर भी कुछ घंटों या दिनों के लिए किताबें लेकर पढऩा, एक-दूसरे से उधार लेकर पढऩा अभी भी दुनिया में बड़े पैमाने पर चलन में है, और इसी निजी मालिक की किताब के मुकाबले लाइब्रेरी की किताब शायद सौ-सौ गुना इस्तेमाल होती है।
ऐसा इसलिए भी होता है कि जिस किताब की जरूरत रहती है, लाइब्रेरी से उस वक्त उसे ही लिया जाता है। अब पश्चिम में एक नया चलन शुरू हो रहा है अपनी जरूरत के किसी भी सामान को सीमित समय के लिए किराए पर लेना। यह एक किस्म से सामानों की लाइब्रेरी है। अभी ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने वहां की एक रिपोर्ट छापी है जिसमें बच्चों के जूते-कपड़ों से लेकर मशीनी औजारों तक, और रसोई के उपकरणों तक तमाम किस्म की चीजें किराए पर मिल रही हैं, और लोग उनका भरपूर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि कुछ लोग अगर घूमने के लिए अपनी जगह से बहुत अधिक ठंडी या गर्म जगह पर जा रहे हैं, तो उसके लिए अलग तरह के कपड़े, जूते, और बाकी तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है। अब इन्हें अगर खरीद लिया जाए तो हफ्ते-दस दिन के बाद उनका कोई इस्तेमाल नहीं रह जाता, और वे सामान बोझ बनकर रह जाते हैं। उपकरणों का इस्तेमाल तो बहुत ही कम होता है, और उन्हें भाड़े पर लाकर काम चलाना एक समझदारी की बात होती है। यह कुछ उसी किस्म का है कि अपनी डिजिटल सामग्री को रखने के लिए हार्डडिस्क खरीदने के बजाय इंटरनेट पर क्लाउड-स्पेस किराए पर ले लिया जाए, और जितनी सामग्री, जितने समय तक वहां रखी जाए, उसके किराए का ही भुगतान किया जाए। यह कुछ वैसा ही है जैसा कोल्ड स्टोरेज में आलू-प्याज, या दूसरी सब्जियां रखने वाले लोगों के साथ होता है, अपने कुछ हफ्तों या महीनों के लिए गोदाम बनाने के बजाय कोल्ड स्टोरेज किराए पर लेते हैं।
मैंने कुछ बरस पहले अपने इसी कॉलम में ‘दस का दम’ नाम की एक कल्पना लिखी थी, लेकिन उस पर आगे कोई काम नहीं हो पाया। सोच यह थी कि लोग अपने आसपास के दस परिवारों का जिम्मा लें कि उनके घरों पर बिना जरूरत रह गए सामानों को दान पर देने की प्रेरणा उन्हें दें, उन सामानों को लेकर किसी एक जगह इकट्ठा करें, और फिर उन्हें जरूरतमंद लोगों को बांट दें। हर परिवार में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के इस्तेमाल के ऐसे बहुत से सामान रहते हैं, जो कि आगे जाकर बेकार रह जाते हैं। दूसरी तरफ समाज के बहुत से जरूरतमंद लोगों को इन चीजों की जरूरत रहती है। ऐसे में एक औपचारिक या अनौपचारिक संगठन की शक्ल में अगर लोग महीने में कुछ घंटे अपने परिचित दस-दस परिवारों से ऐसे सामान जुटाकर उन्हें एक साथ कहीं रखकर जरूरतमंद लोगों को दे सकें, तो गरीबों की बहुत सी जरूरत भी पूरी होगी, और धरती पर नए सामानों का बोझ भी बढऩा थमेगा। मेरी कल्पना यह थी कि दस-दस लोगों के ऐसे समूह बनते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, और जिस तरह आज मार्केटिंग नेटवर्क के सामानों को खपाने के लिए लोगों की एक चेन बनाई जाती है, वैसी चेन नेक काम के लिए भी बनाई जा सकती है।
एक बार अगर कोई भरोसेमंद संस्था ऐसा करके दिखा दे, तो बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कि अपने गैरजरूरी सामान लाकर छोडऩे भी लगेंगे। संस्था और संगठन का फायदा यह होता है कि जरूरतमंद लोगों की शिनाख्त आसानी से, और बेहतर तरीके से हो सकती है। यह सिलसिला शुरू करने के लिए बस दस उत्साही लोगों की जरूरत है, जो कि अपने आसपास के दस, या अधिक परिवारों को सहमत कराकर उनसे उनके लिए गैरजरूरी हो चुकी चीजें ले सकें। धीरे-धीरे इनमें से हर कोई अपने नीचे की, दस-दस लोगों की एक लाईन तैयार कर सकते हैं, और जिस तरह नेटवर्क मार्केटिंग के लोग बढ़ावा देते हैं, वैसे ही अधिक समर्पित समाजसेवी ऐसा ही बढ़ावा दे सकते हैं।
आज धरती पर सामानों की बढ़ती खपत, धरती पर कार्बन का बोझ बढ़ा रही है। नया सामान बनने में चीजें भी लगती हैं, और ऊर्जा भी लगती है, प्रदूषण भी होता है। दूसरी तरफ पुराना सामान कचरे या घूरे में जाकर धरती पर बोझ बनता है। समझदारी इसी में है कि किसी सामान का अधिक से अधिक बार इस्तेमाल कैसे किया जाए? ऐसे में एक तरफ तो हमारा सुझाया जा रहा ‘दस का दम’ जैसा एक खयाल है, दूसरी तरफ ब्रिटेन की आई हुई यह खबर है जिसमें सामानों की लाइब्रेरी की बढ़ती हुई लोकप्रियता बताई गई है। आज भी हिन्दुस्तान में स्कूलों के फैंसी ड्रेस के लिए बच्चों के तरह-तरह के कपड़े बाजार में किराए पर मिलते हैं, और दावतों में जाने के लिए बड़ों के महंग कपड़े भी। धरती पर सामानों का बोझ सीमित रखने के लिए यह एक बड़ा योगदान हो सकता है कि लोग कुछ देर की जरूरत के लिए खरीदने पर मजबूर न हों। क्योंकि एक बार के इस्तेमाल के लिए खरीदे गए सामान बाद में रखने की भी दिक्कत रहती है, जगह भी लगती है, पड़े-पड़े सामान खराब भी होते हैं, और फैशन के सामानों के साथ तो यह भी रहता है कि उनकी फैशन बदल जाती है। इसलिए किसी एक सामान के बनाए जाने के बाद उसका अधिक से अधिक बार इस्तेमाल किस तरह हो सकता है, इसकी योजना लोगों को बनानी चाहिए, चाहे यह समाजसेवा के नजरिए से चीजों को दान में जुटाकर जरूरतमंदों में बांटकर की जाए, या फिर किराए पर मुहैया कराकर। जहां तक धरती और पर्यावरण की बात है उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि इन दोनों में से किस तरीके से नए सामान बनना थम रहे हैं, और पुराने सामानों का घूरे पर जाना थम रहा है।
जिन लोगों के पास कुछ खाली वक्त हो, दोस्तों में से किसी एक के पास एक-दो खाली कमरे हों, या कि कोई गोदाम हो, तो अपने-अपने स्तर पर वे सामान जुटाकर, उसका अधिक इस्तेमाल सुनिश्चित करके धरती का, मतलब है कि अपना खुद का भला कर सकते हैं। धरती का क्या है वह तो तमाम इंसानों के चले जाने के बाद भी बनी रहेगी, और पर्यावरण बर्बाद होने से इंसान खत्म होंगे, धरती तो बची रहेगी।
मेरे एक पुराने अखबारनवीस सहयोगी ने हमारे बड़े लंबे साथ की वजह से सम्मान जताते हुए एक बार एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब किसी खबर को लेकर मन में बहुत बड़ी दुविधा रहती है कि क्या किया जाए, क्या करना चाहिए, तो वे यह कल्पना करते हैं कि वैसी दुविधा अगर मेरे सामने होती, तो मैंने क्या किया होता? और कुछ पल में उन्हें सही राह दिख जाती है। अब यह बात एक बहुत ऊंचे दर्जे के सम्मान की है, जिसे पचाना भी मेरे लिए आसान नहीं है। और वैसे तो आज इस जिक्र का भी कोई खास मकसद नहीं है, सिवाय एक बात के कि जब मेरे सामने लिखने को किसी मुद्दे की कमी रहती है, और पिछले एक बरस से यूट्यूब के लिए कैमरे के सामने बोलने को जब कोई मुद्दा नहीं सूझता है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता हूं। सुप्रीम कोर्ट से जजों के किसी फैसले से ही मुद्दा नहीं सूझता, बल्कि वहां पहुंचे हुए मामलों से, दोनों तरफ के वकीलों के तर्कों से, कई चीजों से कोई विषय सूझता है। आज इस कॉलम को लिखने के लिए कुछ ऐसा ही हुआ है। बीच में कई हफ्ते यह कॉलम लिखना नहीं हो पाता, क्योंकि सोचने-विचारने की कोई बात नहीं सूझती।
सुप्रीम कोर्ट में अभी एक मामला पहुंचा है जिसमें निचली अदालत, और हाईकोर्ट, दोनों का फैसला एक सरीखा था, और उसके खिलाफ मुकदमा हारने वाले ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया। पति-पत्नी के बीच झगड़े और घरेलू हिंसा की बात है, और पत्नी ने पुलिस में शिकायत की, निचली अदालत में मामला चला, वहां से पति को एक बड़ा जुर्माना सुनाया गया, और यह जुर्माना हर्जाने-मुआवजे की शक्ल में पत्नी को मिलना था। लेकिन पति के वकीलों का तर्क था कि यह जुर्माना पति की आर्थिक हैसियत के आधार पर नहीं लगना चाहिए, यह घरेलू हिंसा किस दर्जे की थी, उस आधार पर लगना चाहिए। न तो निचली अदालत ने यह तर्क माना, और न हाईकोर्ट ने, अब सुप्रीम कोर्ट के दो जज इस मामले को सुन रहे हैं, और यह तय होगा कि शादीशुदा जोड़े में जो हिंसक साथी है, उसकी आर्थिक क्षमता के आधार पर फैसला दिया जाए, या हिंसा की शिकार साथी को हुए नुकसान के आधार पर?
मैं बरसों से इस बात को लिखते चले आ रहा हूं कि किसी भी जुर्म में सजा या जुर्माना तय करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मुजरिम, और जुर्म के शिकार के बीच दर्जे का क्या फर्क है। हिन्दुस्तान जैसी स्थितियों में देखें तो यह दर्जा औरत और मर्द के फर्क का सबसे पहले होता है जो कि इस मामले में भी दिख रहा है। शादीशुदा जोड़ों में आमतौर पर महिला हिंसा की शिकार होती है, और समाज और परिवार में अपनी कमजोर स्थिति की वजह से, शारीरिक रूप से पुरूष से कमजोर होने की वजह से वह मार खाती ही है, महिला पुरूष को मारे, ऐसा कम ही होता है। इसलिए औरत और मर्द एक पैमाना है दर्जे के फर्क का। दर्जे के फर्क का दूसरा पैमाना भारत में जाति व्यवस्था है, सवर्ण कही जाने वाली जातियां, दलित-आदिवासी समुदायों पर जुल्म करने की अधिक ताकत रखती हैं, और इसीलिए देश में एक बड़ा जायज कानून बनाया गया है जिससे एससी-एसटी समुदाय पर गैर एससी-एसटी के जुल्म होने पर अधिक कड़ी सजा का प्रावधान है। आज के भारत को देखें तो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग भी धार्मिक बहुसंख्यक लोगों की हिंसा के शिकार होने का खतरा उठाते हैं, और जगह-जगह जहां भी भीड़त्या होती है, उनमें दलित-आदिवासी, या अल्पसंख्यक ही आमतौर पर शिकार होते हैं। अब भेदभाव के एक और बड़े पैमाने की चर्चा कर ली जाए, संपन्न और विपन्न के बीच ताकत का बहुत बड़ा फासला रहता है। एक दौलतमंद जब किसी गरीब पर जुल्म करते हैं, तो गरीब को इंसाफ मिलने की गुंजाइश बड़ी कम रहती है।
हमने बार-बार इस बात को लिखा है, और इस कॉलम में भी मैंने कई बार यह लिखा है कि पैसेवाले किसी गरीब के खिलाफ कोई जुर्म करें, जुल्म करें, या ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोग किसी कमजोर के खिलाफ कुछ करें, तो उसके लिए अलग से कड़ी सजा का इंतजाम होना चाहिए, अलग से मोटे जुर्माने का भी। अभी इसी हफ्ते हमने अपने अखबार या यूट्यूब चैनल पर इस बात को दोहराया भी है कि बलात्कार की शिकार अगर कोई गरीब लडक़ी या महिला रहती है, तो उसमें बलात्कारी की दौलत का एक हिस्सा उसे मिलना चाहिए, जो कि बलात्कारी की बीवी, या उसके बच्चों के हिस्से के बराबर का रहे। ऐसा होने पर ही उस बलात्कारी को अपने परिवार के भीतर भी सजा मिलेगी, जब पारिवारिक सदस्यों के संभावित हिस्से से कुछ दौलत कम हो जाएगी। और ऐसा पर्याप्त मुआवजा बलात्कार की शिकार को मिलने से उसकी कुछ हद तक आर्थिक भरपाई हो सकेगी।
हमारा यह ख्याल है कि विदेश में बसा हुआ यह पति अपनी बड़ी दौलत के दम पर सुप्रीम कोर्ट गया जरूर है, लेकिन वहां भी उसकी हार होगी। घरेलू हिंसा में हिंसा कितनी हुई है, इसके साथ-साथ यह बात अनिवार्य रूप से मायने रखती है कि हिंसा करने वाले व्यक्ति की मुआवजा देने और भरपाई करने की ताकत कितनी है। ऐसे में किसी व्यक्ति पर लगाए जाने वाले जुर्माने की रकम अगर कानून में तय कर ली जाएगी, तो वह बड़ा ही नाजायज होगा। किसी के ओहदे, उसकी ताकत, और उसकी आर्थिक संपन्नता, इन सभी चीजों को देखकर इसके हिसाब से ही उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। एक मजदूर अपनी बीवी को पीटने पर शायद कुछ हजार रूपए जुर्माने को भुगते, लेकिन एक करोड़पति अपनी बीवी को पीटने पर कुछ हजार देने लायक नहीं रहता, उस पर जुर्माना उसकी संपन्नता के अनुपात में रहना चाहिए। इसी तरह हमने पहले भी कई बार इस बात पर लिखा है कि अगर कोई अरबपति भूमाफिया किसी गरीब दलित की जमीन पर कब्जा करे, तो भारत की जाति व्यवस्था के हिसाब से भी जुर्माना तय होना चाहिए, और संपन्नता के फासले के आधार पर भी। बहुत संपन्न के खिलाफ तो किसी मामले के खड़े होने की गुंजाइश भी भारतीय लोकतंत्र में कम रहती है, इसलिए किसी तरह अगर मामला अदालती फैसले तक पहुंचे, तो उस पर जुर्माना तगड़ा लगना चाहिए, करोड़पति-अरबपति को सस्ते में छोडऩा उनकी शान के भी खिलाफ होगा, इसलिए गरीब को इंसाफ दिलाने के लिए न सही, दौलतमंद की सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए जुर्माना तो मोटा ही लगना चाहिए।
देखते हैं अदालत में इस मामले पर क्या फैसला होता है, प्राकृतिक न्याय की हमारी साधारण समझ हिंसा के दर्जे से ऊपर, संपन्नता के आधार पर जुर्माने की वकालत करती है।
पश्चिमी मीडिया की खबरें इस बात से पटी हुई हैं कि किस तरह अमरीका इजराइली हमले के शिकार फिलीस्तीन के गाजा पर पैराशूट से खाना गिरा रहा है। अमरीकी एयरफोर्स की ली गई ऐसी तस्वीरें फैलाई जा रही हैं, और यह भी बताया जा रहा है कि गाजा के किनारे अस्थाई बंदरगाह बनाकर अमरीका वहां से भी मानवीय मदद भेजने की कोशिश कर रहा है। पिछले दो हफ्ते ऐसी खबरों से भरे हुए हैं कि अमरीका इजराइल से इस बात को लेकर खफा है कि वह फिलीस्तीन में मानवीय मदद जाने नहीं दे रहा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों का कहना है कि फिलीस्तीन में लोग अब भूख से मरने की कगार पर हैं, और कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का कहना है कि अनगिनत फिलीस्तीनी बच्चे गाजा में भूख से मर चुके हैं। ऐसे में इजराइल रफा नाम के उस सरहदी शहर पर फौजी कार्रवाई करने पर अड़ा हुआ है जहां पर गाजा के दस लाख से अधिक लोग शरणार्थी बनकर तम्बुओं में पड़े हुए हैं।
अमरीका एक तरफ तो इजराइल के साथ अपनी नाराजगी दिखा रहा है, उससे असहमति दिखा रहा है, और ये खबरें आ रही हैं कि गाजा से हजार मील दूर कतार के एयरफोर्स अड्डे पर अमरीकी वायुसेना के मालवाहक विमानों में भूखे गाजा पर बरसाने के लिए खाने को लादा जा रहा है जिसके बक्से पैराशूट से वहां गिराए जा रहे हैं। इसे कुछ दूसरे पश्चिमी देशों के साथ मिलकर एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना-अभियान की तरह चलाया जा रहा है, और अमरीका यह भी गिना रहा है कि वह गाजा के मलबे पर 40 हजार लोगों के लिए खाने को तैयार पैकेट गिरा रहा है। भूख का हाल यह है कि इसी हफ्ते पानी में गिर गए खाने के बक्सों को निकालते हुए गाजा में 12 लोग डूबकर मर गए, और 6 लोग खाने पर झपटती हुई भीड़ के पैरोंतले कुचलकर मारे गए। ऐसे में इजराइल रफा के शरणार्थी शिविर पर फौजी कार्रवाई के लिए अड़ा हुआ है, जबकि अमरीका इसे गलत करार दे रहा है।
अब तक की इन बातों से लोगों को ऐसा धोखा हो सकता है कि अमरीका में एकाएक तथाकथित इंसानियत आ गई है, और अब वह समंदर के रास्ते, हवाई जहाजों से फिलीस्तीन में खाना भेज रहा है। लेकिन इस गलतफहमी या खुशफहमी को खत्म होने में अधिक वक्ता नहीं लगा। दो दिन पहले 29 मार्च को यह खबर आई कि अमरीका ने इजराइल को नई फौजी मदद मंजूर की है, और दो-दो हजार पौंड के 18 सौ बम, और पांच सौ पौंड के 5 सौ बम इजराइल के लिए और मंजूर किए हैं। इजराइल की सारी गुंडागर्दी सिर्फ अमरीकी मदद पर चलती है, और एक तरफ अमरीका भूख से मरते गाजा पर खाना बरसाने का नाटक कर रहा है, और दूसरी तरफ फिलीस्तीन पर बरसाने के लिए इजराइल को और बम दिए जा रहा है। मतलब यह कि दो-दो हजार पौंड के 18 सौ बम गाजा का जो हाल करेंगे, उसके बाद अमरीका को वहां खाना बरसाने की जरूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि वहां इंसान भी नहीं बचेंगे।
दो-तीन हफ्ते पहले ही मैंने फेसबुक पर लिखा था कि अमरीका एक तरफ इजराइल को 10 लाख छुरे भेज रहा है, और फिलीस्तीन को मरहम की एक हजार ट्यूब। और पिछले हफ्ते-दस दिन में यह बात सही साबित हुई कि भूखों के लिए खाना पहुंचाने के नाटक से अपने लिए शोहरत और हमदर्दी, साख और वाहवाही जुटाने वाले अमरीका ने इजराइल के हाथ इतने मजबूत कर दिए हैं कि वह गाजा की बाकी बची तमाम इमारतों को जमीन से मिला सकता है। आज अमरीका की हालत यह है कि राष्ट्रपति जो बाइडन के इस फैसले का विरोध अमरीका के बहुत से इंसाफपसंद लोग कर रहे हैं, और तो और खुद बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत से नेता और सांसद इसके खिलाफ हैं कि अमरीका इस दर्जे की जारी इजराइली गुंडागर्दी में उसके हाथ मजबूत करने के लिए बम भेजे। दरअसल अमरीका के साथ-साथ बाकी दुनिया में भी अमनपसंद लोग इस बात पर हक्का-बक्का हैं कि पिछले बरस 7 अक्टूबर को एक फिलीस्तीनी आतंकी संगठन हमास के फौजी हमले में सैकड़ों इजराइलियों के कत्ल के बाद जवाब में इजराइल ने अब तक गाजा में 32 हजार से अधिक लोगों को मार डाला है, और पूरे गाजा शहर को मलबे में तब्दील कर दिया है। आधी से अधिक आबादी शरणार्थी शिविरों में पड़ी हुई है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की युद्धविराम की दर्जन भर अपील भी इजराइल के खूनी हमलों को धीमा भी नहीं कर पा रही है।
अमरीका इन दिनों दो अलग-अलग मोर्चों पर उजागर हो रहा है। फिलीस्तीन पर इजराइली फौजी हमले में वह इजराइल को बम और फिलीस्तीनियों को फूड पैकेट देकर दुनिया में जाने किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के मोर्चे को देखें, तो अमरीकी अगुवाई में पश्चिमी देशों के फौजी संगठन, नाटो की तरफ से जितनी फौजी और बाकी किस्म की रसद यूक्रेन को दी जा रही है, वह उसे रूस के हमलों के सामने डटाए रखने के ही काम आ रही है, बचाए रखने के काम नहीं आ रही। अमरीका और योरप के बाकी देश जिस अंदाज में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, उससे एक बात जाहिर है कि वे यूक्रेन को बचाना नहीं चाह रहे, वे रूस को खोखला करना चाह रहे हैं, और अपने इस मकसद के लिए वे कितने भी यूक्रेनी सैनिकों और नागरिकों की मौत देख रहे हैं, पूरे यूक्रेन को मलबे में तब्दील होते देख रहे हैं, और एक गैरबराबरी की जंग में नापतौल कर यूक्रेन की उतनी ही मदद कर रहे हैं जितने से वह मोर्चे पर डटे रहे। नतीजा यह है कि यूक्रेन के कंधों पर बंदूक रखकर पश्चिमी देश रूस पर हमला कर रहे हैं, और रूसी हमले को झेलने के लिए यूक्रेनी सीनों को सामने कर दे रहे हैं।
इस खतरनाक खेल को समझना चाहिए। अमरीका जिस तरह जानलेवा जख्म देने के लिए छुरे सप्लाई कर रहा है, और उसके बाद दुनिया के दिखावे के लिए मरहम भी भेज रहा है, उससे दुनिया के इतिहास में अच्छी तरह दर्ज इजराइल-समर्थक अमरीकी-वीटो मिट नहीं जाएगा। यह भी लगता है कि अमरीका के पास कुछ ऐसा खाना बचा हुआ होगा, जो सडऩे वाला होगा, और उसे गाजा पर बरसाकर अमरीका अपने घूरों का बोझ बढ़ाने से बच रहा होगा। अमरीका की सारी हमदर्दी को, चाहे वह गाजा हो, चाहे यूक्रेन, इस हिसाब से ही समझने की जरूरत है। इजराइल की सारी गुंडागर्दी दुनिया के नक्शे पर बाकी देशों के बीच उसकी मौजूदगी की वजह से मिलने वाली अमरीकी मदद और उकसावे से चलती है, और उसमें ताजा इजाफा करने के लिए अमरीका ने बमों के साथ-साथ फाइटर जेट भी दिए हैं। अभी-अभी का यह ताजा फैसला बमों के साथ-साथ फाइटर जेट भी इजराइल भेज रहा है, और अमरीका को तो चाहिए कि बेघर हो चुके, मां-बाप खो चुके फिलीस्तीनी बच्चों के लिए वह खिलौने के फाइटर प्लेन भी भेज दे, ताकि वह दुनिया के इतिहास में गिना सके कि उसने इजराइल को कम, और फिलीस्तीन को अधिक फाइटर प्लेन दिए थे। इस पूंजीवादी, विस्तारवादी, फौजी-आतंकी साजिश को न समझने वाले अमरीका को मदर टेरेसा भी मान सकते हैं जो कि बिना मां-बाप के रह गए, हाथ-पैर खो चुके फिलीस्तीनी बच्चों की सेवा के लिए फूड पैकेट लेकर गाजा में है।
(शीर्षक: दुष्यंत कुमार का लिखा हुआ)
पिछले कुछ हफ्तों के सुप्रीम कोर्ट को देखें तो लगता है कि केन्द्र और कई राज्य सरकारें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में संविधान और कानून से लगातार टकरा रही हैं। राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के जाने कितने ही फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट को इन सरकारों को याद दिलाना पड़ रहा है कि वे कानून के खिलाफ काम कर रही हैं। ऐसा भी नहीं कि इन्हें अपने दायरे मालूम न हों, क्योंकि निर्वाचित नेता तो नासमझ और बदनीयत हो सकते हैं, लेकिन लगातार काम करने वाले नौकरशाह और बड़े-बड़े सरकारी वकील तो कानून को जानते हैं, और वे पहले से बता सकते हैं कि कौन से फैसले अदालती कटघरे में खड़े नहीं हो सकेंगे। इसके बावजूद अगर सरकारें ऐसे फैसले लेती हैं, ऐसे काम करती हैं, तो यह जाहिर है कि वे अदालत से इन कामों के रद्द या खारिज होने के पहले तक के वक्त का इस्तेमाल करती हैं। चुनावी बॉंड का मामला ऐसा ही रहा, और कई राज्यों की सरकारों के बहुत से फैसले ऐसे ही रहे जिनके बारे में अदालत से खारिज होना तय था, लेकिन उसके पहले तक उनका बेजा इस्तेमाल ही पूरा मकसद था।
अब ऐसा लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, और न्यायपालिका नाम के जो तीन स्तंभ अलग-अलग बनाए गए थे, उनमें से कार्यपालिका किसी बिफरे हुए सांड की तरह नथुनों से फुंफकारते हुए, सींगों से हमला करते हुए जनहित को कुचल देने के लिए टूटी पड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट है कि अपने काम के बाकी बोझ को किनारे रखकर इस सांड को सींगों से थामकर काबू में करने में लगा हुआ है। और तो और, चुनाव आयोग से लेकर राष्ट्रपति तक, राज्यपालों से लेकर विधानसभाध्यक्षों तक जो स्वतंत्र और स्वायत्त संस्थाएं होनी चाहिए, वे सारी की सारी सरकार के मातहत विभागों की तरह काम कर रही हैं। नौबत इतनी खराब हो गई है कि जनता को अब सिर्फ एक संस्था, अदालत की तरफ देखना पड़ रहा है, लेकिन यह लोकतंत्र इस नौबत के लिए बनाया नहीं गया था कि बाकी तमाम संस्थाएं गैरजिम्मेदारी करें, गलत करें, और सिर्फ अदालत उसे सुधारने का काम करे।
देश और प्रदेशों को देखें तो यह साफ है कि सरकारें ऐसे बहुत से फैसले ले रही हैं जिनके बारे में हम उसी वक्त से यह लिखते आए हैं कि वे अदालती सवालों को नहीं झेल पाएंगे, लेकिन सरकारें हैं कि बेझिझक और बेधडक़ होकर ऐसा ही काम करती जा रही है। कहीं आतंक के कानून का ऐसा इस्तेमाल किसी खास तबके की गिरफ्तारी के लिए किया जा रहा है, तो कहीं केन्द्र और राज्य सरकारों की जांच एजेंसियों का काम सत्ता को नापसंद लोगों की गिरफ्तारी तक सीमित रह गया है। राज्यों में भी छांट-छांटकर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामले-मुकदमे दर्ज करने का काम चल रहा है। और सरकारें इस बेशर्मी के साथ ऐसे काम कर रही हैं कि यह भी लगता है कि क्या सरकारों को सचमुच ही कोई अधिकार होना चाहिए?
देश के कानून एकदम साफ हैं, और सरकारों को उनकी सीमाएं मालूम हैं, लेकिन सौ फीसदी गलत तरीके से काम करना जारी है, और सिर्फ निर्वाचित सरकारें नहीं, राज्यपाल और विधानसभाध्यक्ष भी ऐसे खराब और घटिया फैसले ले रहे हैं, कि उन्हें मालूम है कि अदालत उन्हें पलट देगी। लेकिन इसमें कुछ हफ्तों या महीनों का समय लगेगा, और उस वक्त का इस्तेमाल तोडफ़ोड़ करने, सत्ता पलटाने, दलबदल करवाने में किया जाता है। अदालती फैसलों से सरकारें कुछ भी नहीं सीख रही हैं, वे इस बात पर पूरी तरह अड़ी हुई हैं कि उन्हें अदालतों से टकराव लेना है, और मनमानी करनी है। सरकारें तो सरकारें, स्टेट बैंक जैसे सार्वजनिक संस्थान भी सुप्रीम कोर्ट के सामने बेशर्मी से हुक्मउदूली कर रहे हैं, और इसके चेयरमैन तक को अदालत का कोई डर नहीं है।
चुनावी बॉंड से लेकर पीएम केयर्स तक बहुत से ऐसे फंड हैं जिन्हें सरकार जनता की नजरों से दूर रखने पर अड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में तो सरकार ने एक जाति सर्वे करवाया, और उस रिपोर्ट को दो-दो राज्यपाल मानते रह गए, लेकिन किसी को दिया नहीं गया। जनता के पैसों और उन पैसों से किए गए काम का हिसाब भी देना नेता और पार्टियां नहीं चाहते। लोकतंत्र में जनता एकदम ही खारिज कर दी गई है, और जनहित, जनभावना, जनसरोकार जैसे शब्द मानो 21वीं सदी के भारत के इस तथाकथित अमृतकाल के शब्दकोश से निकाल ही दिए गए हैं। ये तमाम बातें लोगों के मन में सवाल खड़े करती, लेकिन ये मन धर्म और जाति की भावनाओं में घिरे हुए हैं, और उनकी बाकी समझ धीमी पड़ चुकी हैं।
जिस रफ्तार से दलबदल चल रहे हैं, और लोग थोक में दलबदल करके सदस्यता खोने से भी बच जा रहे हैं, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अभी चार दिन पहले ही बड़ी हैरानी जाहिर की थी, देखना है कि अदालती जुबानी जमाखर्च किसी फैसले की शक्ल में पहुंच पाएगा या नहीं। इन दिनों देश में जो कुछ अच्छा होते दिख रहा है, वह सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से चल रहा है, क्योंकि कई हाईकोर्ट तो पत्थरयुग और गुफाकाल के अंदाज में काम कर रहे हैं।
भारतीय लोकतंत्र को कुछ थमकर इस पर सोचने की जरूरत है जो कि एक फिल्म के गाने में पूछा गया था- ये कहां...., आ गए हम...
पंजाब में 2022 में वहां के एक लोकप्रिय गायक सिद्धू मुसेवाला का एक गिरोह ने साजिश के साथ बड़ी तैयारी से कत्ल कर दिया था। सिद्धू अपने मां-बाप का इकलौता बेटा था। अब उसके बूढ़े मां-बाप ने उसकी याद में, और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से एक बेटे को जन्म दिया है। सिद्धू के 60 बरस के पिता बलकौर सिंह ने सोशल मीडिया पर बेटे के साथ अपनी फोटो पोस्ट की है, और कहा है कि सब स्वस्थ हैं। पंजाब में बड़े-बड़े गिरोह काम करते हैं, और उनके सरगना तिहाड़ जैसी जेल में रहकर भी अपना गिरोह चलाते हैं, या विदेश में रहकर भी। लेकिन पंजाब के ऐसे संगठित अपराध पर चर्चा उतनी अहमियत नहीं रखती जितनी अहमियत यह बात रखती है कि बुजुर्ग हो चुकी एक महिला किस तरह 58 बरस की उम्र में अपने बेटे की याद में एक और बेटे को जन्म देती है। भारत में शायद कुछ कानूनी अड़चन के चलते ऐसा गर्भधारण करना मुमकिन नहीं था तो सिद्धू मुसेवाला की मां चरणकौर ने दूसरे देश में यह मेडिकल मदद ली। यह अपने किस्म का पहला मामला नहीं है जिसमें एक महिला इस उम्र में मां बने, लेकिन यह कुछ अनोखा मामला तो है ही क्योंकि दुनिया की साधारण समझबूझ यह सुझाती है कि इस उम्र में मां-बाप बनना उतनी समझदारी की बात नहीं है।
अपने बेटे की याद में कुछ करना अच्छी बात है, लेकिन यह भी समझने की जरूरत है कि इंसान के शरीर और उसकी जिंदगी की कुछ सीमाएं रहती हैं, और लोगों को उनका ख्याल इसलिए रखना चाहिए कि जिन बच्चों को मां-बाप अपनी भावनात्मक जरूरतों से पैदा करते हैं, उन्हें बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े होने में खासा समय लगता है, और तब तक उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए मां-बाप की उम्र तो बची होनी चाहिए। वैसे तो बच्चों को जन्म देना हर किसी का मौलिक अधिकार होना चाहिए, लेकिन जब कोई देश एक जनकल्याणकारी राज्य की तरह काम करता है, तो वहां पर अजन्मे बच्चों के अधिकारों की भी फिक्र करनी चाहिए।
आज 60 बरस की उम्र में अगर कोई पिता बना है, और 58 बरस की उम्र में कोई मां बनी है, तो उनकी अपनी जिंदगी का कितना लंबा ठिकाना रहेगा? यह जरूर हो सकता है कि परिवार संपन्न होने पर बच्चे की देखरेख के लिए पैसों का इंतजाम तो पुख्ता हो सकता है, लेकिन मां-बाप दोनों की उम्र अगर बुढ़ापे में दाखिल हो चुकी है, तो उनके अभी हुए बच्चे की जिंदगी के पहले 20-25 बरस मां-बाप के साथ की कोई गारंटी नहीं दिखती है। यहां पर आकर अगर कोई देश कृत्रिम गर्भाधान तकनीक के इस्तेमाल के लिए कोई उम्र सीमा तय करते हैं, तो वह निजी मामलों में दखल नहीं मानी जानी चाहिए।
हिन्दुस्तान में हमने सरोगेसी का कानून आने के ठीक पहले तक कई फिल्मी सितारों को इस तकनीक से बच्चे पैदा करते देखा है, और कुछ तो ऐसे भी रहे जिनके पहले से पर्याप्त बच्चे थे, लेकिन उन्होंने इस तकनीक से और बच्चे हासिल किए। सरोगेसी जैसी तकनीक को लेकर पूरी दुनिया में कई तरह की सोच है, और कई तरह के कानून हैं। यह सिर्फ हिन्दुस्तान में नहीं हैं, बल्कि बहुत सी जगहों पर लोगों को दूसरे देशों में जाना पड़ता है, क्योंकि अपनी खुद की जमीन पर उन्हें इसकी इजाजत नहीं रहती है।
लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए एक सवाल यह सूझता है कि क्या अपनी गर्भ किराए पर देकर अगर कोई बहुत गरीब महिला नौ महीनों बाद अपने परिवार का बेहतर ख्याल रख सकती है, तो क्या उसकी इजाजत दी जानी चाहिए? यह एक समय बिकने वाली किडनी से कुछ अलग मामला है। बदन में किडनी सीमित रहती हैं, और एक किडनी जरूरतमंद मरीज को दे देने पर अपने खुद के बदन पर कई तरह के खतरे आ जाते हैं, और कई तरह की सीमाएं बाकी जिंदगी पर लागू हो जाती हैं। दूसरी तरफ किसी महिला का गर्भाधान उसके लिए उतना बड़ा खतरा नहीं रहता, और उसकी बाकी जिंदगी पर इसकी वजह से कोई बहुत बुरा असर नहीं पड़ता। फिर अपनी कोख किराए पर देना किसी तरहसे अंगदान जैसा नहीं है कि जिससे शरीर के किसी हिस्से को बेचने का काम हो जाए। आज जब देश में भुगतान की क्षमता वाले लोग हैं, और सबसे गरीब लोग पैसों की कमी से एक सामान्य जिंदगी नहीं जी पाते हैं, उनके बच्चे अभाव में बड़े होते हैं, किन्हीं अवसरों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में भारत के मौजूदा सरोगेसी कानून के तहत क्या ऐसी कोई ढील नहीं देनी चाहिए जिससे गरीब परिवारों की महिलाएं किसी बच्चे को जन्म देकर अपने खुद के बच्चों के लिए एक अच्छी रकम जुटा सकें? यह बात सुनने में अमानवीय लग सकती है कि हम कोख किराए पर देने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन यह बात किसी महिला की अपनी और उसके परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाने की बात भी है, साथ-साथ बिना बच्चों वाले लोगों के लिए एक मौका मुहैया कराने की बात भी है।
हिन्दुस्तान जैसे मुल्क की इस हकीकत को नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में महिलाएं अपने बच्चों को कुपोषण से मरते देखती हैं, बिना इलाज बच्चे बड़े सब मर जाते हैं, छोटे-छोटे बच्चे सडक़ों पर कचरा बीनने और भीख मांगने जैसे रोजगार में लगने को मजबूर रहते हैं। और इससे भी अधिक कड़वी हकीकत यह भी है कि ह्यूमन राईट्स वॉच नामक संस्थान के एक अंदाज के मुताबिक हिन्दुस्तान में करीब डेढ़ करोड़ महिलाएं देह बेचने के धंधे में लगी हुई हैं। एशिया का सबसे बड़ा सेक्स बाजार मुम्बई है जहां पर एक लाख से अधिक वेश्याएं काम करती हैं। सरकारें इन आंकड़ों को न जानना चाहती हैं, न मानना चाहती हैं, लेकिन जब अपनी जिंदगी और परिवार को चलाने के लिए इस देश में डेढ़ करोड़ महिलाएं दुनिया में सबसे अधिक बीमारियों के खतरे वाला यह धंधा करती हैं, तो क्या इसके मुकाबले किसी के बच्चे की मां बन जाना अधिक बुरा काम होगा?
चूंकि वेश्यावृत्ति को कानूनी हक देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार और संसद को इस बारे में कुछ नहीं करना पड़ा, इसलिए वे असुविधा से बचे हुए हैं। लेकिन चूंकि सरोगेसी को लेकर संसद को कानून बनाना पड़ा है इसलिए सरकार और संसद उस मामले में ऐसे दिखना नहीं चाहते कि वे बदन को किराए पर देने का समर्थन कर रहे हैं। जबकि शरीर को कुछ मिनटों या घंटों के सेक्स के लिए किराए पर देने का कारोबार सबकी जानकारी में है, और उसे मानते कोई भी नहीं हैं।
हमने बात तो सिद्धू मुसेवाला के मां-बाप के बच्चे के फैसले को लेकर शुरू की थी, लेकिन वह आगे बढक़र इस तकनीक पर आ गई है, और किस तरह इस तकनीक से कुछ कमाने की इजाजत लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि वे अपने बदन के कई और अधिक बुरे इस्तेमाल कर ही रहे हैं। आज भी हिन्दुस्तान में किडनी ट्रांसप्लांट जैसे कारोबार में कानून को चकमा देकर किडनी की खरीद-बिक्री चलती ही है। संसद में पिछले बहुत समय से किसी कानून को लेकर सार्थक चर्चा और बहस का सिलसिला खत्म हो गया है, इसका नतीजा यह हुआ है कि कई ऐसे कानून भी बन जाते हैं जो कि जायज नहीं होते। सरोगेसी कानून का गरीबों के जिंदा रहने के लिए किस तरह इस्तेमाल हो सकता है इस पर बात होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट अभी यह देखकर हक्का-बक्का रह गया कि राजस्थान में एक महिला के कत्ल के मामले में पुलिस ने उसकी नाबालिग बेटी को ही प्रताडि़त करके फंसाने की कोशिश की, और उसे ही हत्यारा बनाकर कोर्ट में पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने राजस्थान के पुलिस प्रमुख को मामले की जांच करके रिपोर्ट देने कहा है कि एक बच्ची पर किस तरह गुनाह कबूलने को जुल्म करके उसे तैयार किया गया कि वह मां का कत्ल करना मान ले। चौदह बरस की इस बच्ची के साथ पुलिस के रवैये पर जज हैरान थे। और बच्ची को फंसाने का यह काम हत्यारे के साथ मिलकर पुलिस ने किया था। मामले के खुलासे को पढऩा दहशत पैदा करता है कि किस तरह लडक़ी को फंसाने के लिए पुलिस ने साजिश रची, और उसे मार-मारकर यह कबूलवाया कि उसी ने मां को गोली मारी थी।
दुनिया भर के सभ्य देशों में बच्चों को सिखाया जाता है कि वे खतरा देखें, या परेशानी में पड़ें, तो वे सीधे पुलिस के पास जाएं। बच्चों को भरोसा दिलाया जाता है कि पुलिस हर नौबत में हर तरह से उनकी मदद करेगी। दूसरी तरफ हिन्दुस्तान में जमीनी हकीकत देखते हुए बच्चों को यह ठीक ही समझाया जाता है कि वे समय पर सो जाएं, समय पर खाना खा लें, वरना पुलिस उन्हें उठाकर ले जाएगी। आज पुलिस के बीच से कुछ लोग अच्छा काम करते भी दिखते हैं, कहीं किसी भूखे को खिलाते हैं, तो कहीं किसी बुजुर्ग को सडक़ पार कराते हैं, लेकिन देश भर में पुलिस का आम हाल इतना खराब है कि लोग उससे दूर रहने में ही अपना भला मानते हैं। जाने कितने ही मामले ऐसे हुए हैं जिनमें अदालत के सामने पुलिस मुजरिम और गुंडा साबित हो चुकी है। असल जिंदगी में तो लोग देखते ही हैं कि संगठित अपराधों को इजाजत देने के लिए पुलिस खुद एक संगठित अपराधी की तरह काम करती है। भारत के अधिकतर प्रदेशों में पुलिस सत्ता के हाथ का हथियार बनी रहती है, और अगर सत्ता की दिलचस्पी पुलिस के बेजा इस्तेमाल में न भी हो, तो भी पुलिस अपने आपको हथियार की तरह पेश करती है। अभी कुछ ही दिन पहले साम्प्रदायिक हिंसा से गुजर रहे उत्तराखंड में एक मुस्लिम मोहल्ले में एक हिन्दू की लाश मिली, जिसकी तोहमत जाहिर तौर पर मुस्लिमों पर ही लगनी थी। लेकिन उसी प्रदेश की पुलिस ने जांच करने पर पाया कि वहीं के एक स्थानीय हिन्दू पुलिसवाले ने एक निजी रंजिश निकालने के लिए एक हिन्दू नौजवान का कत्ल किया, और उसकी लाश को मुस्लिम मोहल्ले में फेंक दिया था। सुबूत मिल जाने पर इस पुलिसवाले को गिरफ्तार किया गया है। ठीक ऐसा ही एक दूसरा मामला उत्तरप्रदेश में एक जगह सामने आया था जहां पर एक हिन्दू संगठन के लोगों ने अपने अवैध कारोबार को बेरोकटोक चलाने के लिए उस इलाके के पुलिस अफसर का तबादला करवाने की योजना बनाई, और इसके लिए गाय काटकर जगह-जगह उसके टुकड़े फेंके गए, उनके साथ एक बेकसूर मुस्लिम का नाम जोड़ा गया, उसका आईडी कार्ड साथ डाल दिया गया। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने ही हिन्दू संगठन की यह साजिश पकड़ी, और तमाम लोगों को गिरफ्तार किया, इसके बाद नाजायज गिरफ्तार बेकसूर मुस्लिम को रिहा किया गया।
पुलिस जगह-जगह सबसे परले दर्जे के संगठित मुजरिमों की तरह काम करने के लिए एक पैर पर तैयार खड़ी रहती है। और ऐसा करने वाले लोगों की गिनती अपवाद सरीखी नहीं है, पुलिस का एक खासा हिस्सा भ्रष्टाचार में तो डूबा रहता ही है, वह बेकसूरों को फंसाने, और मुजरिमों को बचाने में भी लगा रहता है। हमने मुम्बई के बड़े चर्चित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिसवालों को देखा है कि वे किस तरह आगे चलकर भूमाफिया बन जाते हैं, और बंदूकबाज होने की अपनी शोहरत का इस्तेमाल करके मुजरिमों की सरगना बन जाते हैं। हिन्दुस्तानी कानून व्यवस्था में पुलिस को जुर्म दर्ज करने और गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई के लिए अंधाधुंध अधिकार मिले हुए हैं, और यह उसका एकाधिकार सरीखा रहता है। इसलिए उससे बचना बड़ा मुश्किल रहता है। राजनीतिक ताकतें अपने बुरे लोगों को बचाना, और विरोधियों को झूठे मामलों में फंसाना इन्हीं पुलिसवालों के सहारे करती हैं। अधिकतर जिलों और थाना इलाकों में अवैध कमाई और उगाही का जमा जमाया कारोबार रहता है, और ऐसी कमाऊ कुर्सियों पर पहुंचने के लिए पुलिस अपने आपको औजार और हथियार की तरह पेश भी करती है, और मोटी पेशगी भी देती है।
ऐसे भ्रष्ट सिलसिले को तोडऩा जरूरी है। यह सिलसिला जारी रहे तो राजनेता इसके आदी भी हो जाते हैं, क्योंकि पेशेवर भ्रष्ट पुलिसवाले उन्हें यह भी समझा देते हैं कि वे कैसे विरोधियों को निपटा सकते हैं, कहां-कहां से कमा सकते हैं। ऐसी पुलिस कभी-कभी अदालत के सामने उजागर होती है, तो फंसती है, आमतौर पर निचली अदालतों का मिजाज ही ऐसा रहता है कि वहां पुलिस या सरकार जो मामला पेश करे, उन्हें अदालतें सच और सही मानकर चलती हैं। राजस्थान का यह मामला देश में पुलिस की बदनामी का न तो पहला मामला है, न आखिरी है। पंजाब में केपीएस गिल जैसे अफसर के मातहत जिस तरह सैकड़ों बेकसूर लोगों की पुलिस-हत्या के आरोप लगे थे, और बाद में दर्जनों पुलिसवालों को अदालत से सजा भी हुई थी, उसे भी नहीं भूलना चाहिए। अभी दो दिन पहले ही दिल्ली में एक नमाजी को पुलिस ने जिस तरह मारा है, उसे भी नहीं भूलना चाहिए। पुलिस सत्ता की चापलूस बनकर हर तरह के जुर्म करने को तैयार रहती है, और इसके सबसे बुरे शिकार सबसे कमजोर तबके होते हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)