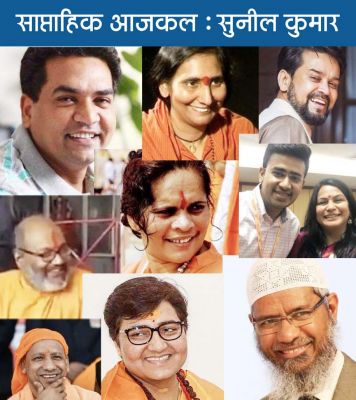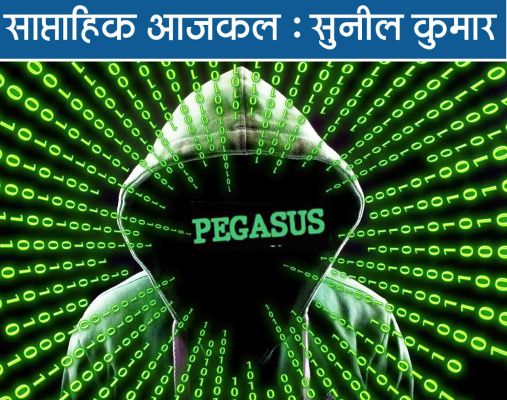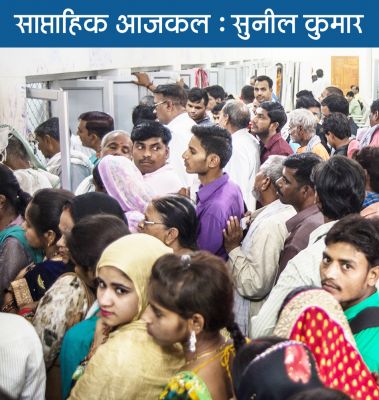आजकल
ब्रिटिश राजघराने के राजकुमार प्रिंस हैरी और उनकी गैर गोरी पत्नी मेगन मार्कल ने जब राजघराने से अलग होने की घोषणा की, जब ब्रिटेन से बाहर जाकर अमरीका में बसने की घोषणा की, अपनी राजकीय उपाधियां लौटा दीं, तो वे लोगों को कुछ अलग लगे थे। किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि शाही शान-शौकत को छोडक़र कोई महज संपन्न और आम इंसान की तरह दूसरे देश में जाकर रहना पसंद करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिखाया। वैसे भी यह शादी अपने आपमें अटपटी थी क्योंकि मेगन मार्कल पहले एक बार शादीशुदा रह चुकी थीं, और अश्वेत भी थीं, ये दोनों बातें ब्रिटेन की शाही परंपराओं के साथ माकूल नहीं बैठती थीं। लेकिन इस शाही जोड़े ने और भी कई बातों में आम लोगों की तरह रहना तय किया था, और अपनी संपन्न जिंदगी के बावजूद वे राजघराने की सामंती जिंदगी से परे अमरीका के कैलिफोर्निया में रह रहे हैं। लेकिन अभी एक ऐसी बात हुई जिससे इनके गैरसामंती मिजाज पर एक सवाल उठ खड़ा हुआ है।
मेगन मार्कल ने अभी अमरीकी सरकार में एक अर्जी दी है कि वे अपने पॉडकास्ट के लिए आर्कटाइप (Archetypes) नाम छांट रही हैं, और इस शब्द का इस्तेमाल और लोगों के लिए प्रतिबंधित किया जाए। इस शब्द का मतलब दुनिया भर में समझा जाने वाला एक ऐसा प्रतीक या शब्द, या ऐसा बर्ताव होता है जिसकी कि और लोग नकल करते हैं। यह शब्द आमतौर पर पौराणिक कथाओं से निकली मिसालों में इस्तेमाल होता है। अब मेगन मार्कल ने अपने ऑडियो प्रसारण के पॉडकास्ट के लिए यह नाम छांटा है जो कि प्राचीन ग्रीक भाषा से आया हुआ है, और अंग्रेजी में सन् 1540 से जिसके इस्तेमाल का रिकॉर्ड मिलता है। अब मेगन की अर्जी के मुताबिक बाकी तमाम लोगों को इस शब्द का इस्तेमाल करने से रोका जाए, और इसका ट्रेड मार्क अधिकार उसे दिया जाए।
अमरीका की कारोबारी दुनिया में इस किस्म के कानूनी दावे और उनको मिलने वाली चुनौतियां बहुत आम बात है। लेकिन आर्कटाइप शब्द तो कई दूसरी अमरीकी कंपनियों के नाम में है, उनके सामानों के नाम में है। कुछ कंपनियों के ट्रेडमार्क में यह शब्द पहले से चले आ रहा है, और उनका यह हक बनता है कि वे मेगन मार्कल की इस अर्जी को चुनौती दें। इस बात की जिक्र करने का आज का मकसद महज यह है कि जो नौजवान जोड़ा एक तरफ तो सामंती जिंदगी से बाहर आ चुका है, और दूसरी ओर सैकड़ों बरस से प्रचलन में चले आ रहे एक आम शब्द पर इस तरह का दावा करना कुछ ऐसा ही है कि मानो हिन्दुस्तान में कोई खट्टा-मीठा नमकीन नाम का एक ब्रांड उतार दे, और फिर ऐसे पेटेंट का दावा करे कि कोई और प्रोडक्ट खट्टा-मीठा या नमकीन शब्द का इस्तेमाल न कर सकें।
राजघराने की शान-शौकत से अपने आपको अलग कर लेना भी कोई छोटी बात नहीं थी। दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राजघराना, उसके परंपरागत ओहदों के साथ इतनी अहमियत जुड़ी हुई है कि उन्हें छोडऩा शायद ही किसी के बस का रहता हो। फिर भी प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल ने ऐसा कर दिखाया। लेकिन उनका यह नया दुराग्रह उनके कारोबारी हितों के हिसाब से तो ठीक है क्योंकि अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग को इंटरनेट पर पॉडकास्ट की शक्ल में देने के एवज में इस भूतपूर्व शाही जोड़े को सैकड़ों करोड़ रूपए मिलने जा रहे हैं। इसके लिए जो कारोबारी अनुबंध हुआ है, किसी आवाज के लिए उतना बड़ा अनुबंध कभी हुआ नहीं था। ऐसे में इनका मैनेजमेंट देखने वाले एजेंट तो ऐसा जरूर चाहेंगे कि इनके कार्यक्रम का जो नाम है, उस नाम का इस्तेमाल कोई और न करे, लेकिन जब उसमें हैरी-मेगन की सहमति हो जाती है, तो फिर यह सवाल भी उठता है कि एकाधिकार की ऐसी सामंती चाह क्या जायज है? सैकड़ों बरस से अंग्रेजी भाषा में जो शब्द बना हुआ है, उस शब्द के इस्तेमाल पर इस किस्म के एकाधिकार की सोच भी नाजायज है। हर देश में नामों के इस्तेमाल को लेकर तरह-तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, अखबारों और पत्रिकाओं के नाम, टीवी चैनलों और वेबसाइटों के नाम अलग-अलग रजिस्टर होते हैं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता कि किसी एक प्रचलित आम शब्द को लेकर हर किस्म का रजिस्ट्रेशन किसी एक के नाम कर दिया जाए। खासकर तब जबकि उस नाम से पहले ही कुछ कंपनियां चल रही हैं, और कुछ प्रोडक्ट उस नाम से बाजार में हैं।
आज दुनिया का कारोबार इस किस्म की बहुत सी तिकड़मों का रहता है। अमरीका में जहां पर कानून का पालन बड़ा कड़ा है, वहां पर बड़ी-बड़ी कंपनियों को भी अपनी छोटी-छोटी टेक्नालॉजी, डिजाइन, और सामान को लेकर पेटेंट दफ्तर जाना पड़ता है, और जरा-जरा सी चीज का पेटेंट करवाना पड़ता है। चूंकि वहां पर इस कानून को तोडऩे पर बड़े लंबे जुर्माने का नियम है, इसलिए लोग इसे तोडऩे से बचते हैं, और इसीलिए लोग तरह-तरह के पेटेंट करवाने में भी लगे रहते हैं ताकि उससे होने वाला हर किस्म का कारोबारी फायदा उन्हें अकेले ही मिले। लेकिन सैकड़ों बरस पुराने आम प्रचलन के एक शब्द पर कारोबारी एकाधिकार कुछ अधिक ही सामंती मांग है, और इससे यह भी तय होगा कि अमरीका का कानून ऐसे दूसरे मामलों में भी क्या रूख रखेगा।
चिकित्सा वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि लोग बाहर से जो जूते-चप्पल पहनकर आते हैं, अगर उन्हें पहनकर वे घर भर में घूमते रहते हैं तो घर में बीमारियां आने का खतरा अधिक रहता है। बाहर सडक़ें और सार्वजनिक जगहें आमतौर पर साफ नहीं रहती हैं, और जूते-चप्पल के साथ कई किस्म की गंदगी आती है, जो कि घरों में किसी और तरह से नहीं आ सकती है। इसलिए कई किस्म के कीटाणु और रोगाणु घर में लेकर आने का काम जूते-चप्पलों से होता है। इसलिए न सिर्फ हिन्दुस्तान के परंपरागत रीति-रिवाजों में, बल्कि जापान, चीन, और रूस जैसे बहुत से देशों में भी जूते-चप्पल बाहर उतारने का रिवाज है, फिर लोग चाहें तो घरों के भीतर के लिए अलग रखी हुई चप्पलें पहन लें। हिन्दुस्तान में कई दुकानों और दफ्तरों में भी ऐसा लागू किया जाता है, बाहर नोटिस लगा दिया जाता है कि जूते-चप्पल बाहर उतारें, लेकिन जूते या सैंडल खोलते हुए उनमें लगने वाले हाथ धोने का इंतजाम शायद ही कहीं रहता है, मंदिरों तक में नहीं रहता है, और लोग ऐसे गंदे हाथों से ही भीतर जाते हैं, कहीं फूल चढ़ाते हैं, कहीं प्रसाद पाते हैं, या किसी के घर-दुकान में सामने परोसे गए नाश्ते को उन्हीं हाथों से खाते हैं। कुल मिलाकर मतलब यह है कि अगर जूते-चप्पल बाहर उतरवाने हों, तो उन्हें उतारने-पहनने के बाद हाथ धोने का कोई इंतजाम होना चाहिए, वरना वह न उतारने से भी अधिक नुकसानदेह हो सकता है।
भारत में भी अब शहरीकरण और संपन्नता बढऩे के साथ-साथ लोग घर के कालीन पर भी लोगों का जूतों सहित आना उनके गर्मजोशी से स्वागत का एक हिस्सा मानते हैं। फिर चाहे ऐसा कालीन महीनों तक साफ न होता हो, और जूतों की लाई गंदगी उनमें समाई रहे। लोगों को धार्मिक भावना से नहीं, सेहत की भावना से यह ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अभी तो पिछले दो बरस से कोरोना की मार चल रही है, और आने वाले बरसों में हो सकता है कि गंदगी से फैलने वाली बीमारियां फैलने लगें, और उस दिन जूते-चप्पल की आदत बड़ा नुकसान कर जाए।
इस छोटी सी बात पर लिखने की जरूरत इसलिए लग रही है कि आज जिंदगी में बीमारियों का खतरा और इलाज का खर्च जिस रफ्तार से बढ़ते चल रहे हैं उन्हें देखते हुए बचाव ही अधिकतर लोगों के लिए अकेला इलाज हो सकता है। लोगों को रोज की जिंदगी में साफ-सफाई, सेहतमंद बने रहने के आसान प्राकृतिक तरीके, खानपान की सावधानी, तनावमुक्त जिंदगी जैसी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे कम बीमार पड़ें, और इलाज की नौबत न आए। आज भी हम अपने आसपास के लोगों को देखें तो किसी भी उम्र के लोगों को जितने किस्म की महंगी बीमारियां हो रही हैं, उनका खर्च कितना होता होगा, उनके काम का कितना हर्ज होता होगा, इसका अंदाज बाकी लोगों को हिला सकता है।
दुनिया के दो विकसित देशों में एक बात एक सरीखी है। चीन और जापान इन दोनों में लोग सुबह नहीं नहाते, वे काम से लौटने के बाद घर पहुंचकर नहाते हैं। इसका तर्क बड़ा आसान है कि दिन भर घर के बाहर रहकर काम करके लोग तरह-तरह के प्रदूषण के साथ लौटते हैं, और संक्रमण के खतरे के साथ भी। इसके बाद इसी तरह खाकर सो जाने से वह प्रदूषण और संक्रमण बदन पर करीब चौबीस घंटे ही बने रहता है। इससे बेहतर यह है कि बाहर से घर लौटने पर नहाया जाए, और फिर अगले दिन घर के बाहर जाने पर प्रदूषण और संक्रमण का सामना शुरू होने तक तो कम से कम साफ-सुथरे रहें। एक चिकित्सा विशेषज्ञ का यह भी कहना है कि लोग बाहर से जब आते हैं, तो वे हवा में तैरते पराग कणों को भी अपने साथ ले आते हैं, और उनके बदन और कपड़ों से वे पराग कण घर के सोफे या बिस्तर पर भी चले जाते हैं, और परिवार के उन दूसरे लोगों को भी परेशान करते हैं जिन्हें उनसे एलर्जी है। इसलिए बाहर से आकर नहाने और कपड़े बदल लेने में ही सेहत के लिए एक बड़ी समझदारी है।
अब रोज के कामकाज को अगर देखें, तो अधिकतर लोगों को हर दिन घंटे भर का वक्त मिल सकता है, योग-ध्यान, प्राणायाम, कसरत, या सैर करने के लिए। गरीब से लेकर अमीर तक अलग-अलग लोगों के लिए इनकी संभावनाएं अलग-अलग हो सकती हैं लेकिन सबसे गरीब लोग भी किसी खुली जगह पर या आसपास के बगीचे में घंटे भर पैदल चल सकते हैं, और इससे सेहतमंद बने रहने में मदद मिलती है जिससे कि कई किस्म की बीमारियों का खतरा कुछ कम होता है। गरीब की जिंदगी में खतरा कम होना ही सबसे बड़ी बचत है क्योंकि आज जिस रफ्तार से बीमारियां बढ़ रही हैं, उसी रफ्तार से इलाज और दवाएं भी बढ़ रही हैं, और लोग कर्ज लेकर भी इलाज तो कराते ही हैं। लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि जब वे सेहतमंद बने रहने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए रोजाना इस तरह के बचाव की जीवनशैली अपनाते हैं, तो वे बिना कहे हुए अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक मिसाल भी बन जाते हैं, और अपने बच्चों को वे विरासत में सावधानी दे जाते हैं। फिटनेस के लिए महंगे जिम जरूरी नहीं हैं, मामूली चप्पल-जूतों के साथ भी किसी खुली जगह पर, किसी सडक़ के किनारे सुबह-शाम की सैर की जा सकती है, या खाली हाथों भी कसरत की जा सकती है जिसके लिए कोई मशीनें नहीं लगतीं।
बचाव के ही सिलसिले में एक बात और लिखने को रह जाती है कि लोगों को सिगरेट-तम्बाकू, शराब जैसी आदतों से बचना चाहिए क्योंकि इनमें न सिर्फ इस्तेमाल के पहले खरीदने का भारी खर्च होता है, बल्कि इस्तेमाल के बाद कई किस्म की बीमारियों की गारंटी रहती है, जिनसे इलाज हो पाना हर बार मुमकिन भी नहीं होता। परिवार में एक किसी को कैंसर हो जाए तो मामूली कमाई वाला तो पूरा परिवार ही तबाह हो जाता है। इसलिए दोनों किस्म के खर्च बचाने के लिए, सेहत ठीक रखने के लिए, और परिवार को मुसीबत में न डालने के लिए लोगों को इन बुरी आदतों से पूरी तरह बचना चाहिए। यह बात इसलिए भी जरूरी है कि बुरी आदतों वालों के बच्चे भी इन आदतों का खतरा रखते हैं, और किसी भी समझदार या जिम्मेदार को अपनी अगली पीढिय़ों को ऐसी विरासत नहीं देनी चाहिए।
आज जब चारों तरफ बहुत से जलते-सुलगते मुद्दे हैं, तब भी जिंदगी के इन बुनियादी मुद्दों पर लिखने की जरूरत इसलिए है कि हर वक्त आसपास अनगिनत लोगों को बचाने की जरूरत तो बनी ही रहती है। ये बातें सावधानी की फेहरिस्त की कुछ बातें ही हैं, लोग बाकी बातें खुद सोच सकते हैं, या किसी से पूछ सकते हैं। एक बार जब मिजाज सावधानी का हो जाता है, तो दिल-दिमाग जिंदगी के बाकी पहलुओं को भी तौलने-परखने लगते हैं। तो चलिये कुछ बातों से तो सावधानी शुरू करें, जूते-चप्पल घर के बाहर उतारें, और मुमकिन हो तो काम खत्म करके लौटने पर नहा लें।
इंसान की मुस्कुराहट के क्या मायने हो सकते हैं, इसका एक नया नजरिया दिल्ली के हाईकोर्ट के एक जज ने अभी एक बहुत ही संवेदनशील मामले की सुनवाई के दौरान सामने रखा है। दिल्ली दंगों से जुड़े हुए एक मामले की सुनवाई जस्टिस चंद्रधारी सिंह की अदालत में चल रही है, और इसमें सीपीएम सांसद रहीं बृंदा करात ने मोदी सरकार के एक मंत्री अनुराग ठाकुर के एक बयान पर यह मुकदमा किया है। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी के वोट मांगते हुए मंच से नारा लगाया था- देश के गद्दारों को..., और इसके बाद उन्होंने आम सभा की भीड़ को इसे पूरा करने का मौका दिया था जिसने आवाज लगाई थी-गोली मारो सालों को।
यह वीडियो चारों तरफ खूब फैला था, और इसे लेकर बीते दो बरसों में यह मामला अदालत में चल रहा है और उसकी सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि अगर मुस्कुराते हुए कोई बात कही जाए तो उसके पीछे आपराधिक भावना नहीं रहती, लेकिन अगर कोई बात तल्ख लहजे में कही जाए तो उसके पीछे की मंशा आपराधिक हो सकती है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि चुनाव के समय दी गई स्पीच को आम समय में कही बात से नहीं जोड़ा जा सकता। चुनाव के समय अगर कोई बात ही है तो वह माहौल बनाने के लिए होती है, लेकिन आम समय में यह चीच नहीं होती, उस दौरान माना जा सकता है कि आपत्तिजनक टिप्पणी माहौल को भडक़ाने के लिए कही गई थी।
जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने एक मुस्कुराहट को जिस तरह की रियायत दी है वह हैरान करने वाली है, और भयानक है। लोगों को याद होगा कि हिन्दी फिल्मों के बहुत से खलनायकों के नामी किरदार हत्या से लेकर बलात्कार तक हँसते-हँसते करते आए हैं। दुनिया की सबसे हिंसक फिल्मों में भी कई ऐसी रही हैं जिनमें ऐतिहासिक हिंसक पात्र दिल हिला देने वाली हिंसा हँसते-मुस्कुराते करते दिखे हैं। एक अमरीकी फिल्म में एक मानवभक्षी आदमी पुलिस हिरासत में रहते हुए भी पुलिस की जरा सी चूक से एक पुलिस वाले पर कब्जा कर लेता है और उसे मारकर खा लेता है। वह भी फिल्म के कई हिस्सों में मुस्कुराते हुए दिखता है। इसलिए देश में घोर साम्प्रदायिक नफरत फैलाने वाली, हिंसा फैलाने वाली बातें अगर चुनावी भाषणों में की जाती हैं, और जिनके असर से इस देश में कमजोर मुस्लिमों के कत्ल का माहौल बनता है, उन्हें देश का गद्दार करार दिया जाता है, तो ऐसे फतवों को भी एक मुस्कुराहट की वजह से मंजूरी देने वाली जज की यह बात बहुत ही भयानक है, और उनकी कमजोर समझ, और बेइंसाफ सोच को उजागर करती है। इंटरनेट पर उनका परिचय बताता है कि वे छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के वक्त सरकार द्वारा मनोनीत अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाए गए थे।
दो दिन पहले बृंदा करात के दायर किए गए मुकदमे में जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने फैसला सुरक्षित रखा है और यह सवाल किया है कि इस भाषण में साम्प्रदायिक नीयत कहां है? जज के खड़े किए हुए कई और सवाल भी लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों को विचलित करने वाले हैं क्योंकि वे देश की बुनियादी धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को खारिज करने वाली बातों को एक मुस्कुराहट का फायदा दे रहे हैं। अगर उनकी यह बात उनके लिखित फैसले में किसी तरह आती है, और अगर उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, तो इंसाफ की हमारी सीमित बुनियादी समझ यह कहती है कि जस्टिस चंद्रधारी सिंह की इस व्याख्या पर सुप्रीम कोर्ट नहीं मुस्कुराएगा। पता नहीं जस्टिस सिंह ने फिल्म शोले देखी थी या नहीं जिसमें गब्बर अपने आधे जुर्म हँसते हुए करता है, अपने साथियों को गोली मारने सहित। अब अगर वह फिल्म न होती और मामला आज का होता तो गब्बर अपनी हँसी और मुस्कुराहट को लेकर आज संदेह का लाभ पाने का हकदार रहता।
जब देश की बड़ी अदालतों के जज कानून की ऐसी व्याख्या करने लगें, तो हिंदुस्तानी लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी फिक्र खड़ी हो जाती है। इस मामले में और कुछ न सही, जस्टिस चंद्रधारी सिंह को कम से कम यह तो देखना था कि इस चुनावी भाषण को लेकर जनवरी 2020 में चुनाव आयोग ने अनुराग ठाकुर को देश के गद्दारों को वाले नारे के लिए नोटिस जारी किया था और आयोग ने नोटिस में यह लिखा था कि पहली नजर में यह टिप्पणी साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाडऩे का खतरा रखने वाली दिखती है और भाजपा सांसद ने आदर्श चुनाव संहिता और चुनाव कानून का उल्लंघन किया है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह को कम से कम यह तो सोचना था कि चुनाव प्रचार के दौरान का भडक़ाऊ भाषण न सिर्फ साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाडऩे का खतरा रखता है, बल्कि वह लोकतंत्र के फैसले को भी गलत तरीके से मोडऩे का खतरा रखता है।
हिंदुस्तान की न्यायपालिका का हाल के कुछ बरसों का रूख दिल बैठा देने वाला रहा है। बहुत से ऐसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं जिनके फैसले, आदेश, या जिनकी टिप्पणियां लोकतंत्र को कुचलने वालों को संदेह का लाभ देने वाली रही हैं, और लोकतंत्र का हौसला पस्त करने वाली रही हैं।
यह भी एक दिलचस्प बात है कि आज जब हिंदुस्तान में दिल्ली हाईकोर्ट के ये जज इस मामले में फैसला सुरक्षित रखकर बैठे हैं, उस वक्त अमरीका में सुप्रीम कोर्ट की जज बनाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक काली महिला की संसदीय समिति के सामने सुनवाई चल रही है। अमरीका में किसी के सुप्रीम कोर्ट जज बनने के पहले सभी पार्टियों के सदस्यों को मिलाकर बनाई गई कमेटी इस संभावित जज से कई-कई दिनों तक खुली सुनवाई में उसकी पूरी जिंदगी, सोच, विचार, उसके फैसले, सभी के बारे में सैकड़ों सवाल करती है और यह माना जाता है कि यह दुनिया की सबसे कड़ी पूछताछ में से एक रहती है। अमरीका में देश और समाज के जो जलते-सुलगते मुद्दे रहते हैं, उन पर भी ऐसे संभावित जजों की सोच पूछी जाती है, धर्म, राजनीति, समाज से लेकर गर्भपात पर तक उनके पिछले बयानों को लेकर उनसे खूब पूछताछ होती है।
हिंदुस्तान में जब-जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी ऐसी असाधारण सोच सामने रखते हैं, तो लगता है कि क्या इस देश में भी किसी को बड़ा जज बनाने के पहले उससे उसकी जिंदगी, उसकी सोच, उसके पिछले कामकाज के बारे में सार्वजनिक पूछताछ नहीं होनी चाहिए? आज अमरीका में इस काली महिला से चल रही पूछताछ का जीवंत प्रसारण चल रहा है, और हर अमरीकी को यह जानने का हक है कि उनके राष्ट्रपति ने देश की बड़ी अदालत में जज बनाने के लिए किस तरह के व्यक्ति को मनोनीत किया है, और ऐसी खुली सुनवाई में कौन से सांसद कौन से सवाल कर रहे हैं? लोकतंत्र इसी तरह की खुली पारदर्शिता का नाम है।
हिंदुस्तान में अब बड़े जज रिटायर होने के बाद कोई किसी राजभवन चले जाते हैं, तो कोई राज्यसभा। रिटायर होने के ठीक पहले के सूरजमुखी फैसलों के बाद इस तरह का वृद्धावस्था-पुनर्वास न्यायपालिका की साख को वैसे भी चौपट कर चुका है। आज हिंदुस्तान में भी जरूरत है कि किसी के हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज बनाने जाने के पहले उनकी ऐसी ही खुली सुनवाई हो, जैसी कि अमरीका में हर जज की होती ही है।
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रधारी सिंह की टिप्पणी पर देश के एक चर्चित मुस्लिम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है-तेरा मुस्कुराना गजब हो गया...।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
दुनिया में खुशी की सालाना रिपोर्ट का यह दसवां साल है। हर बरस यह रिपोर्ट बनती है कि किस देश के लोग सबसे अधिक खुश हैं। पिछले कई बरसों से लगातार यह देखने में आता है कि योरप के स्कैंडेनेवियाई कहे जाने वाले देश सबसे अधिक खुशहाल देश हैं। और यह बात महज संपन्नता से जुड़ी हुई नहीं है, यह संपन्नता के साथ-साथ वहां के लोगों की मानसिक स्थिति और सामाजिक वातावरण जैसे कई पैमानों को भी बताती है। लिस्ट में सबसे ऊपर योरप के देशों का ही बोलबाला है, फिनलैंड सबसे ऊपर है, फिर डेनमार्क, आइसलैंड, स्विटजरलैंड, और नीदरलैंड्स हैं। लेकिन इस लिस्ट में भारत का हाल देखें तो वह दुनिया के देशों में 139वें नंबर पर है। 2018 में वह एक 133वें नंबर पर था, अब वह 139वें पर आ गया है। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि 2013 में जब यूपीए सरकार थी तब लोगों की खुशी के पैमाने पर भारत दुनिया में 111वें नंबर पर था, और अब वह फिसलकर 139वें पर पहुंचा है, मतलब यह कि लोग अब खुश नहीं हैं।
दूसरी तरफ यह भी देखने की जरूरत है कि हिन्दुस्तान किन देशों के आसपास खड़ा हुआ है। हिन्दुस्तान के आसपास की लिस्ट देखें तो उसके तुरंत बाद के देशों में तमाम देश अफ्रीका के हैं, यमन और अफगानिस्तान जैसे बदहाल देश हैं जो कि भुखमरी की कगार पर हैं। हिन्दुस्तान के पड़ोस के सारे ही देश हिन्दुस्तान से अधिक खुशहाल जिंदगी जीने वाले पाए गए हैं, कम से कम वहां की आबादी हिन्दुस्तान के मुकाबले अधिक खुश है। इस लिस्ट में पाकिस्तान 103 नंबर पर है, नेपाल उसके भी ऊपर 85 नंबर पर है, चीन 82 नंबर पर है, और हिन्दुस्तान के दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश 99 नंबर पर है, इराक 109 नंबर पर है, इरान 116 नंबर पर है, म्यांमार 123 नंबर पर है, श्रीलंका 126 पर है। इतने तमाम देश के लोग अपने आपको हिन्दुस्तानियों के मुकाबले अधिक खुश पाते और बताते हैं।
इस रिपोर्ट को दुनिया में लोगों की खुशी और खुशहाली को आंकने का एक सबसे अच्छा औजार माना जा रहा है, इसमें किसी देश का दर्जा तय करते हुए प्रति व्यक्ति, सामाजिक सुरक्षा, औसत उम्र, जिंदगी में पसंद की आजादी, उदारता, और भ्रष्टाचार के प्रति नजरिया जैसी बातों पर आंकलन किया जाता है। इस लिस्ट में भारत की भारी गिरावट की कई वजहें पाई गई हैं। यह देश दुनिया के दवा-उद्योग की राजधानी माना जाता है, यहां दुनिया भर से चिकित्सा-पर्यटन पर लोग आते हैं, लेकिन यह अपने नागरिकों को इलाज मुहैया कराने में, औसत उम्र के मामले में दुनिया में 104 नंबर पर है। इस लिस्ट में सबसे आखिरी 146वें नंबर पर अफगानिस्तान हैं, और बदहाली की इस लिस्ट में हिन्दुस्तान उससे बस 10 सीढ़ी बेहतर है।
अब इन आंकड़ों का क्या मतलब निकाला जाए? 2013 में जब यूपीए सरकार थी, उस वक्त अगर हिन्दुस्तान दुनिया के 110 देशों से बदहाल था, तो आज वह 136 देशों से अधिक बुरी हालत में है। लोग खुश क्यों नहीं है? लोगों को तो आज एक उग्र राष्ट्रवाद मिला हुआ है, जिसकी वजह से एक साकार या निराकार दुश्मन को देखते हुए उनका कलेजा अधिक ठंडा होना चाहिए था, लेकिन वैसा दिख नहीं रहा है। आज हिन्दुस्तानियों की जिंदगी में धर्म जिस तरह घोल-घोलकर पिला दिया गया है, उससे भी लोगों को भारी खुश रहना चाहिए था, लेकिन वे वैसे खुश दिख नहीं रहे हैं। यह भी एक अजीब बात है कि योरप के जो देश इस लिस्ट में सबसे अधिक खुश दिख रहे हैं, उन देशों में धर्म का महत्व घटते चले जा रहा है, चर्च के भूखों मरने की नौबत आ गई है, और लोग धर्म से परे की जिंदगी में बहुत खुश हैं। तो क्या हिन्दुस्तान में आज का धार्मिक उन्माद लोगों की जिंदगी की खुशियों को बढ़ाने के बजाय घटा रहा है?
इस रिपोर्ट को भी और बहुत सी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट की तरह खारिज किया जा सकता है कि यह भारत को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है कि धार्मिक उन्माद में लगे हुए आबादी के एक छोटे हिस्से की वजह से बाकी तमाम आबादी एक नाजायज तनाव और खतरे से गुजर रही है, और उसकी जिंदगी की खुशियां कम हो गई हैं? यह बात समझने के लिए तो किसी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट की जरूरत भी नहीं है, और भारतीय समाज के अमन-पसंद लोगों की बहुतायत से बात करके ही इसको समझा जा सकता है। एक तरफ धार्मिक उन्माद, धर्मान्धता, नफरत, और उसके साथ-साथ बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई। कोई हैरानी नहीं है कि हिन्दुस्तान में पहले से अधिक लोगों में खुशी पहले से कम है।
आज जब धर्म के नाम पर इस देश को बांटा जा रहा है, लोगों को नफरत सिखाई जा रही है, और आबादी का एक छोटा लेकिन नारेबाज हिस्सा लगातार भडक़ाऊ और हिंसक बातें पोस्ट कर रहा है, तब यह उन्माद किसी में खुशी नहीं भर सकता। किसी तबके, धर्म या जाति से नफरत का मतलब खुशी नहीं हो सकता, उन्माद और हिंसा का मतलब खुशी नहीं हो सकता। हाल के बरसों में हिन्दुस्तान ने अभूतपूर्व धर्मोन्माद देखा है, असाधारण साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण देखा है, ऐसा उग्र राष्ट्रवाद हिन्दुस्तान ने कभी देखा नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि इन सबने मिलकर भी इस देश को खुशी नहीं दिला पाई है। यह देश तमाम सामाजिक और आर्थिक पैमानों पर, लोकतांत्रिक और मानवाधिकार के पैमानों पर दुनिया के कम से कम सौ देशों के काफी नीचे है।
हिन्दी के एक सबसे बड़े साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल अपनी रचनाओं से परे एक बार खबरों में हैं। पहले सोशल मीडिया पर एक अभिनेता-लेखक से बातचीत में उनकी कही यह तकलीफ सामने आई कि देश के दो बड़े प्रकाशन समूहों से उन्हें अविश्वसनीय रूप से कम रॉयल्टी मिल रही है। उनकी यह शिकायत भी सामने आई कि उनसे बिना पूछे इन दोनों प्रकाशकों ने उनकी किताबों के ई-बुक संस्करण छापे हैं। उन्होंने कहा कि वे इतने सालों से ठगे जा रहे हैं, और वे अब इन दोनों प्रकाशकों से स्वतंत्र होना चाहते हैं। उनके बताए गए जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक इन दोनों प्रकाशकों से उन्हें सालभर में कुल 14 हजार रूपए मिले हैं जबकि इन दोनों से उनकी पौन दर्जन किताबें छपी हैं जो कि हिन्दी की सबसे चर्चित किताबें रही हैं।
लेकिन सुबूतों के बिना यह कहना मुश्किल है कि प्रकाशकों की यह बात गलत है कि वे सीमित संख्या में ही किताबें प्रकाशित करते हैं जिन्हें लेखक कभी भी आकर जांच सकते हैं, और विनोद कुमार शुक्ल के साथ उन्होंने कोई बेईमानी नहीं की है, उन्हें पूरा हिसाब-किताब भेजा है, और उन्हें अनुबंध के मुताबिक भुगतान किया है। विनोद कुमार शुक्ल का कहना है कि प्रकाशक उन्हें कम रॉयल्टी देकर ठग रहे हैं, और नए संस्करणों की जानकारी भी उन्हें तब दी जाती है जब वे प्रकाशित होकर आ जाते हैं। इस विवाद पर कई और लोगों ने कई बातें कही हैं जो कि लेखक और प्रकाशक के बीच वैचारिक और कारोबारी मतभेद भी बताती हैं, और लेखकों का असंतुष्ट होना भी। इस कारोबार को जानने वाले लोगों का कहना है कि हिन्दी के लेखक को प्रकाशक की तरफ से अधिकतम दस फीसदी रॉयल्टी दी जाती है।
हिन्दी साहित्य की किताबों के कारोबार को अगर समझें तो लेखकों का बड़ा बुरा हाल सुनाई पड़ता है। कुछ दर्जन सबसे कामयाब लेखकों को अगर छोड़ दें, तो अधिकतर लेखक प्रकाशक को भुगतान करके कुछ सौ किताबें छपवाते हैं, और उन्हें 25-50 किताबें अपने करीबी लोगों में बांटने के लिए मिल जाती हैं, और बाकी किताबें प्रकाशक सरकारी या लाइब्रेरी खरीदी के अपने नेटवर्क में खपाने की कोशिश करते हैं। लेखक के संपर्क अगर अधिक होते हैं तो उनकी किताबों की कहीं-कहीं चर्चा हो जाती है, और इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी किताबों का अंधाधुंध प्रचार करके भी हिन्दी के सबसे अधिक चर्चित लेखक भी कुछ हजार किताबों की बिक्री में कामयाब होते हैं। लेकिन रॉयल्टी पाने वाले लेखकों में भी पांच-दस फीसदी रॉयल्टी का मतलब बड़ी छोटी रकम है, जो कि किसी भी लेखक के लिए गुजारे का सामान नहीं है।
यह किसी प्रकाशक ने किसी लेखक से कहा भी नहीं है कि उनकी जिंदगी किताबों की कमाई के भरोसे चल जाएगी, और लेखक भी दूसरों के तजुर्बे से यह बात जानते ही हैं। हम किसी एक लेखक के किसी एक प्रकाशक के साथ अनुबंध की शर्तों के पूरे न होने के बारे में यहां पर नहीं लिख रहे, हम व्यापक तौर पर इस कारोबार के बारे में लिख रहे हैं ताकि हम कारोबार से आगे बढक़र पाठक तक की बात कर सकें।
हिन्दी के बड़े से बड़े लेखक-प्रकाशक की किताबें शायद 30-35 फीसदी कमीशन पर दुकानदार बेचते आए हैं। वह भी तब जब किताबें बिक जाएं। किताब में पहला पूंजीनिवेश वक्त और प्रतिभा का लेखक का होता है, और उसके बाद प्रकाशक का। अच्छे प्रकाशक किताब का संपादन करते हैं, गलतियां सुधारते हैं, लेखक से अनुबंध करके किताब की छपाई करते हैं, मीडिया में किताब के बारे में छपवाने की कोशिश करते हैं, कहीं पुस्तक मेले में या किसी और जगह किताबों का प्रमोशन करते हैं, और दुकानदारों या पुस्तकालयों को उधार में मोटे कमीशन पर किताबें पहुंचाते हैं। यह कारोबार कुछ कच्चा कारोबार है। किसी भी जगह किताबें मौसम या दीमक की शिकार हो सकती हैं, डिलिवरी के दौरान खराब हो सकती हैं, किसी मामले-मुकदमे में फंस सकती हैं, या प्रतिबंधित हो सकती हैं। इन सबका बोझ भी कुल मिलाकर प्रकाशक पर ही पड़ता है। हो सकता है कि इससे परे भी प्रकाशक पर कुछ और बोझ होते हों, और लेखक पर भी कुछ और बोझ होते हों।
अब हम एक पाठक के नजरिए से इस कारोबार को देखें तो लगता है कि प्रकाशक-मुद्रक के स्तर पर सौ रूपए में तैयार होने वाली किताब दुकान के स्तर पर तीन सौ से छह सौ रूपए में जब बिकती है, तो उसके खरीददार कम ही रह जाते हैं। हिन्दी के आम पाठकों की साहित्यिक चेतना और उसके साहित्यिक सरोकार शायद ऐसे नहीं रहते कि जिंदगी के दूसरे खर्चों को कम करके कुछ किताबें खरीदी जाएं। यही वजह है कि हिन्दी के सबसे चर्चित लेखकों में से एक विनोद कुमार शुक्ल की किताबें भी सैकड़ों में ही बिकती हैं, और उनकी सालाना कमाई पन्द्रह हजार रूपए भी नहीं हो पाती है। साहित्य के बजाय राजनीतिक और विवादास्पद मुद्दों पर लिखने वाले हिन्दी लेखकों की कमाई इसके मुकाबले कुछ या कई गुना अधिक हो सकती है, लेकिन वह भी किसी के गुजारे के लिए काफी नहीं हो सकती।
अब सवाल यह है कि जिस लेखन-प्रकाशन कारोबार का सारा दारोमदार एक खरीददार-पाठक पर टिका होता है, वही अगर दो-चार हजार तक भी नहीं पहुंचता, तो यह एक बड़ा नाजुक कारोबार है, फल या सब्जी के धंधे जैसा, या उससे भी अधिक नाजुक। इतने सीमित खरीददारों के भरोसे लेखक भी क्या कर ले, और प्रकाशक भी क्या कर ले? और इन दोनों के बीच की खींचतान जिस छोटी सी कमाई पर टिकी है, वह अपने आपमें बड़ी सीमित और छोटी है। अगर उसमें बेईमानी हो रही है, लेखक का शोषण हो रहा है, तो वह रूपयों की शक्ल में एक छोटा शोषण है।
जब इस देश की आबादी का तकरीबन आधा हिस्सा हिन्दी बोलने वाला माना जाता है, पचास करोड़ से अधिक लोग हिन्दीभाषी हैं, तो उनके बीच हिन्दी साहित्य की किताब हजार-दो हजार भी न बिक पाना कई सवाल खड़े करता है। पहला सवाल तो यही है कि क्या लोग हिन्दी साहित्य खरीदना नहीं चाहते, या फिर वह उनकी पहुंच से दूर है? एक सवाल यह भी है कि क्या हिन्दी साहित्य की किताबों की लागत, और उनकी कीमत का अनुपात सही है? क्या किताबों के दाम काफी कम हो जाने से उनके पाठक-ग्राहक बढ़ सकते हैं? मेरा यह मानना है कि हिन्दी साहित्य की किताबों के दाम इतने अधिक रखे जाते हैं कि लोगों ने धीरे-धीरे उन्हें अपनी सीमा से बाहर मान लिया, और खरीदना बंद कर दिया, शायद धीरे-धीरे पढऩा भी बंद कर दिया। क्या किताबों को सस्ता छापकर, कम कमीशन के रास्ते बेचकर, उनकी अधिक संख्या में बिक्री हो सकती है? यह एक सवाल मुझे बार-बार सताता है कि क्या लेखक प्रकाशकों के चले आ रहे ढर्रे से परे भी कुछ कर सकते हैं ताकि उनकी किताबें कम दाम पर बिकें, और ग्राहक-पाठक बढ़ें?
हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं की किताबों को लेकर सस्ते प्रकाशन के कुछ प्रयोग हुए भी हैं, और जब-जब किताबें कम दाम पर लोगों को मिलती हैं, वे अधिक संख्या में खरीदते हैं, अधिक लोग खरीदते हैं, और अधिक पढ़ते भी हैं। अधिक दाम और सीमित संख्या किसी कारोबार के लिए तो अधिक माकूल हो सकते हैं, लेकिन क्या यह सचमुच ही लेखक के हित में है कि उसका लिखा बस कुछ हजार लोगों तक पहुंचकर सीमित रह जाए?
अब सवाल यह भी है कि प्रकाशक का किताबों की बिक्री का एक नेटवर्क होता है, और वह नेटवर्क किसी एक किताब के लिए खड़ा नहीं किया जा सकता, उसके लिए कई किताबों के प्रकाशक ही कामयाब हो सकते हैं। ऐसे में लेखक अपनी किताब खुद प्रकाशित करे, और उसे बेचे यह भी मुमकिन नहीं लगता। लेकिन प्रकाशकों को खुद अपने हित में भी बहुत कम दाम और कमाई वाली किताबें छापनी चाहिए, ताकि ग्राहक बढ़ सकें, पाठक बढ़ सकें। जब तक ग्राहक-पाठक की यह बुनियाद चौड़ी नहीं होगी, यह कारोबार एक खंभे पर खड़े हुए बड़े से होर्डिंग जैसा रहेगा जिसे वक्त की आंधी कभी भी गिरा देगी।
आज विनोद कुमार शुक्ल की तकलीफ की खबरों से यह लिखने का मौका मिला है, और मेरी यह साफ-साफ सोच है कि समझदार लेखक-प्रकाशक को अखबारी कागज जैसे सस्ते कागज पर, बिना पु_े वाले कवर में किताब छापनी चाहिए, उसे कम कमीशन पर इंटरनेट पर बेचना चाहिए, और अधिक पाठकों को ग्राहक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। महंगी छपाई, महंगी जिल्द से किसी के लिखे हुए की इज्जत नहीं बढ़ती, उसे कितने अधिक लोग पढ़ते हैं, लिखे हुए कि कितने अधिक लोग तारीफ करते हैं, उससे लेखक की इज्जत बढ़ती है। महंगी छपाई और महंगी जिल्द प्रकाशन के कारोबार का एक हिस्सा है, वह लेखन का हिस्सा नहीं है। लेखक को अपनी सीमित किताबें दिखने में खूब अच्छी पाने का लोभ छोडऩा चाहिए। ऐसा सुना है कि इंटरनेट पर अमेजान कुल सत्रह फीसदी कमीशन पर लेखक-प्रकाशक के पते से किताब उठाता है, और देश भर में कहीं भी डिलीवर करता है। इसमें भुगतान भी चार-छह दिनों के भीतर ही हो जाता है। मतलब यह कि यह किताब दुकानों को दिए जाने वाले कमीशन से आधा ही है।
लेखकों को अपने स्तर पर यह सोचना चाहिए कि परंपरागत प्रकाशकों का कोई विकल्प हो सकता है क्या, जो कि उनका (लेखकों का) अधिक भला कर सके? प्रकाशकों को भी सीमित ग्राहकों को महंगी किताब बेचने से परे के विकल्प सोचने चाहिए कि पढऩे की आदत बनाए रखने के मुताबिक कम दाम पर किताबें बेची जाएं, ताकि वे अधिक संख्या में बिकें, और प्रकाशन का कारोबार अधिक संख्या में लोगों पर टिका रहे, अधिक भरोसे का रहे।
किताब को छापने और बेचने का मेरा एक अलग तजुर्बा रहा है जो कि बताता है कि आज के बाजार की हिन्दी साहित्य की अधिकतर किताबें एक चौथाई बाजार भाव पर आ सकती हैं, अगर लेखक-प्रकाशक गैरजरूरी महंगी क्वालिटी के चक्कर में न पड़ें। पूरी दुनिया में आज हर कारोबार सीमित कमाई और असीमित ग्राहकों के मामूली समझ वाले फॉर्मूले पर काम कर रहा है, और जमे हुए प्रकाशक अगर ऐसा करना नहीं चाहते तो कुछ जनसंगठनों को भी इस धंधे में उतरना चाहिए।
न सिर्फ हिन्दुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इन दिनों मीडिया को लेकर एक असमंजस बना हुआ है कि किसे मीडिया गिना जाए, और किसे नहीं। जो लोग अखबारों के वक्त के पुराने बुजुर्ग सोच के लोग हैं, वे आज के इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को लेकर अक्सर उसे नीची नजरों से देखते हैं कि यह कोई पत्रकारिता नहीं है। बात सही भी है, पत्रकारिता शब्द पत्र से बना हुआ है जिसका मतलब समाचार पत्र होता था। एक समाचार पत्र को तैयार करने में धातू के बने हुए टाईप, एक-एक अक्षर, और एक-एक मात्रा को जोडक़र एक-एक वाक्य ढाला जाता था, और बड़ी मुश्किल से एक पेज तैयार हो पाता था। आज मोबाइल फोन या कम्प्यूटर पर बोलकर घंटे भर में उतना टाईप किया जा सकता है, और पल भर में उसे किसी वेबसाईट पर पोस्ट किया जा सकता है। छपे हुए शब्दों को मिटाना मुमकिन नहीं था, और इसलिए लिखने और छपने के बीच खासी फिक्र की जाती थी, बड़ी सावधानी बरती जाती थी। आज अगर कोई गलत बात भी पोस्ट हो जाती है तो उसे पल भर में, कम से कम आम लोगों के लिए तो, मिटाया जा सकता है, उसे बदला जा सकता है।
यह दौर छपे हुए शब्द और बिना छपाई महज इंटरनेट पर पोस्ट किए गए शब्द के बीच मुकाबले का दौर है, और ऐसे में एक परंपरागत विश्वसनीयता, और टेक्नालॉजी की सहूलियत से हासिल लापरवाही के मुकाबले का दौर भी है। सरकारें अधिक से अधिक लोगों को खुश करने के लिए हर उस वेबसाईट को मीडिया मानने पर आमादा हैं जिन्हें घर बैठे कोई भी दो-चार हजार रूपए की लागत से शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद उस पर लिखने या पोस्ट करने वाली किसी भी बात के लिए वे तब तक किसी के लिए जवाबदेह नहीं रहते जब तक कि कोई उनके खिलाफ पुलिस या अदालत तक न जाए, या कि सरकार उनमें से किसी को अपने निशाने पर न लें। यह सिलसिला कुछ अटपटा इसलिए है कि अभी हाल में चल रहे चुनावों के बीच भी कम से कम एक राज्य में ऐसी वेबसाईटों को मीडिया मानने को लेकर एक बड़ी पार्टी ने कई किस्म के वायदे भी किए हैं, और दूसरे कई राज्यों में बिना किसी पत्रकारिता के चलने वाली वेबसाईटों को भी मीडिया का दर्जा देने का काम किया गया है। एक समाचार वेबसाईट बनाना, और उस पर राशिफल-भविष्यफल से लेकर अश्लील वीडियो तक पोस्ट करके हिट जुटाना सरकारों की तकनीकी परिभाषा में एक कामयाब मीडिया हो गया है, और पत्रकारिता के जो परंपरागत नीति-सिद्धांत अखबारों के वक्त, अखबारों के मामले में इस्तेमाल होते थे, वे कूड़ेदान में चले गए हैं।
यह सरकारों और राजनीतिक दलों की अधिक से अधिक लोगों को खुश करने की कोशिश का नतीजा है कि आज घर बैठे, कुछ हजार रूपयों में हर कोई मीडिया बन सकते हैं, और उसके बाद वे मीडिया के लिए तय की गई सरकारी सहूलियतों से लेकर अभिव्यक्ति की आजादी की परिभाषा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे लेकर पहले भी इसी जगह पर हमने कई बार लिखा है कि कम से कम अखबारों को तो मीडिया नाम की इस वटवृक्ष सरीखी विशाल छतरी के बाहर आ जाना चाहिए, और जो लोग अपने आपको मीडिया कहना या कहलाना चाहते हैं उन्हें उनके हाल और उनकी मर्जी पर छोड़ देना चाहिए।
एक वक्त महज प्रेस शब्द इस्तेमाल होता था क्योंकि अखबार प्रेस में छपा करते थे। बाद में धीरे-धीरे जब मीडिया के नाम पर टीवी और दूसरे किस्म के माध्यम जुड़े, तो प्रेस शब्द पता नहीं कब मीडिया बन गया। आज इस शब्द का जितना बेजा इस्तेमाल हो रहा है, और कहीं मीडिया अपनी आत्मा बेचने की तोहमत पा रहा है, तो कहीं गिरोहबंदी करके किसी नेता या सरकार को बढ़ाने की, तो ऐसे में पुरानी फैशन के उस प्रेस को अपने अलग अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए और लौटकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करनी चाहिए।
ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अलग-अलग टेक्नालॉजी की वजह से अलग-अलग किस्म के समाचार या विचार-माध्यम के तौर-तरीके अलग-अलग तय होते हैं। और पुराने अंदाज के छपने वाले अखबारों के तौर-तरीके कभी भी सिर्फ वेबसाईटों पर चलने वाले मीडिया की तरह नहीं हो सकते। बुरे से बुरे और छोटे से छोटे अखबार को भी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए खासी मेहनत करनी पड़ती थी, और यह मेहनत उनके मिजाज और चरित्र में एक गंभीरता लाती थी। वह पूरा सिलसिला आज के मीडिया नाम के विकराल दायरे में खो गया है। और यही वजह है कि अखबारों को अखबार बनकर रहना चाहिए, अपने आपको वापिस प्रेस की परिभाषा के भीतर सीमित रखना चाहिए। सरकारें अपनी मर्जी से जैसा चाहें वैसा करें, लेकिन अखबारों को अपने नीति-सिद्धांतों की उस पुरानी परंपरा पर लौटना चाहिए, क्योंकि उसके बिना न उनकी कोई इज्जत है, और न ही उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई दावा करने का कोई हक है।
जैसा कि दुनिया में अधिकतर कीमती चीजों के साथ होता है, मोती समंदर की गहराई में मिलते हैं, सतह पर तैरते हुए नहीं, हीरों की तलाश करनी पड़ती है, सोना गहरी खदानों में मिलता है, समझ लंबे तजुर्बे से हासिल होती है, मजबूत इमारती लकड़ी देने वाले पेड़ को तैयार होने में सौ-पचास बरस लगते हैं, ठीक वैसे ही अच्छे सामाजिक सरोकार वाले इज्जतदार माध्यम बनने में अखबारों को सौ-पचास बरस तो लगे ही थे। बड़ी मुश्किल से हासिल इज्जत और महत्व का वह दर्जा, और सामाजिक सरोकार की वह भूमिका आसानी से नहीं खोनी चाहिए, और पत्रकारिता को आज की कैमराकारिता, या वेबकारिता से अलग अपने तौर-तरीके तय करना चाहिए।
(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
पिछले कुछ बरसों से दुनिया में एक प्रयोग चल रहा है, और उस पर बहस भी चल रही है। पुलिस के कामकाज को आसान और असरदार बनाने के लिए एक ऐसा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसमें खतरे में पड़े हुए, या खतरनाक लोगों की जानकारी डाली जाती है। इसके अलावा शहरों की उन जगहों की शिनाख्त भी की जाती है जहां पर जुर्म होने का खतरा अधिक है, और उन जगहों को भी शहरी नक्शे पर दर्ज किया जाता है। फिर ऐसी जगहों और ऐसे लोगों के बारे में और अधिक जानकारी जुटाई जाती है, और कम्प्यूटर अपना अंदाज बताता है कि किन लोगों के आसपास, किन जगहों पर जुर्म होने की आशंका अधिक है। इनमें जुर्म करने वाले लोग भी हो सकते हैं, और जुर्म का शिकार होने वाले लोग भी। पिछले करीब दस बरस से अमरीका में इस किस्म का प्रयोग चल रहा है, और इसे वहां की पुलिस काम का भी पा रही है। लेकिन पुलिस से परे के कुछ जानकार विशेषज्ञ इस कार्यक्रम के खतरे भी देखते हैं। इसके तहत जिन लोगों को खतरनाक या खतरे में पाया जाता है, उनसे पुलिस सौ किस्म के सवाल करती है। और ये सवाल उनकी शुरुआती जिंदगी में इस हद तक चले जाते हैं कि अगर उनके मां-बाप का तलाक हुआ था, तो उस वक्त वे किस उम्र के थे।
यह बात एक सामाजिक हकीकत हो सकती है कि विभाजित परिवारों के बच्चों की जिंदगी में खतरे कुछ अधिक हो सकते हैं, और हो सकता है कि पुलिस के रिकॉर्ड यह साबित करने वाले हों कि ऐसे बच्चे समाज के लिए दूसरे बच्चों के मुकाबले कुछ अधिक खतरा ला सकते हैं। लेकिन ऐसी जानकारी जब कानून लागू करने वाली एजेंसियों के हाथ रहेगी तो उनका इस्तेमाल करने वाले लोगों के मन में एक मजबूत पूर्वाग्रह बन जाने का खतरा रहेगा कि कुछ रंगों के लोग, कुछ धर्मों के लोग, कुछ जातियों के लोग, कुछ विभाजित परिवारों के लोग पुलिस की खुर्दबीनी निगाह के नीचे रहेंगे। और ऐसा करने पर यह हो सकता है कि उनके कानून तोडऩे के मामले पुलिस की नजरों में तुरंत आ जाएं, और वे आसानी से मुजरिम साबित किए जा सकें क्योंकि उन पर पहले से नजर रखी जा रही थी, और उनके खिलाफ सुबूत आसानी से जुटे हुए हैं। लेकिन अगर कानून लागू करने वाली एजेंसियां कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर पर आधारित इस किस्म के सामाजिक पूर्वाग्रह से भरी रहेंगी, तो वे एक सामाजिक हिंसा का सबब भी बनी रहेंगी।
लोगों को याद होगा कि अमरीका में हर बरस एक से अधिक ऐसे भयानक चर्चित मामले आंदोलन की बुनियाद बनते हैं जिनमें गोरों के नजरिए से काम करने वाली पुलिस कालों पर हिंसा करती है, उन्हें कुचलती है, उनके हक छीनती है। ऐसी हिंसा के खिलाफ समय-समय पर अमरीकी राष्ट्रपतियों ने भी अफसोस जाहिर किया है। अब अपराध की भविष्यवाणी करने वाली ऐसी प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के कम्प्यूटर प्रोग्राम को अगर भारत पर लागू करके देखें, तो यहां तो आज बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों को लेकर वैसे भी एक हिंसक पुलिस बना चुके हैं। कई राज्यों में पुलिस घोर साम्प्रदायिक हो चुकी है, और सत्ता ने भी जब धार्मिक आधार पर जमकर भेदभाव चला रखा है, तो सत्ता के हाथों नकेल वाली पुलिस के लिए यह आम बात ही है कि वह सत्ता के तलुए सहलाने के लिए उसके राजनीतिक एजेंडे को लागू करे। आज अगर जुर्म करने का खतरा अधिक रखने वाले लोगों की एक लिस्ट पुलिस के हाथ रहेगी तो यह जाहिर है कि वह उसमें से पसंदीदा लोगों को पकडऩे और जेल भेजने के आसान काम में लगी रहेगी। जिस अमरीका को लेकर आज की यह चर्चा शुरू की गई है उस अमरीका का हाल यह है कि वहां के एक बड़े शहर में 2013 में जब यह लिस्ट बनाई गई थी तो उसमें खतरनाक या खतरे में पांच सौ लोगों से कम के नाम थे, और आज दस बरस के भीतर ही ये नाम बढक़र चार लाख से अधिक हो चुके हैं। मतलब यह कि खतरे में, या खतरनाक लोगों का एक ऐसा डेटाबेस पुलिस के हाथ तैयार है जिसे वह अपने नस्लभेदी, रंगभेदी नजरिए के साथ मनमाने तरीके से इस्तेमाल कर सकती है।
फिर लौटकर हिन्दुस्तान की बात पर आएं तो यह समझने की जरूरत है कि यहां नागरिकों की जितने किस्म की जानकारी सरकार रोजाना ही इकट्ठा कर रही है, उससे लोगों की जिंदगी की निजता भी खत्म हो रही है, और वे एक सुनियोजित साजिश का खतरा भी अधिक झेल रहे हैं। इसे इस तरह समझें कि आज किसी जुर्म में पकड़े गए किसी इंसान के आधार कार्ड से पल भर में यह जानकारी निकाली जा सकती है कि उसके परिवार के बाकी लोगों के आधार कार्ड नंबर क्या हैं। इनके अलावा उन नंबरों से इन लोगों के फोन नंबर, एटीएम नंबर, गाड़ी के नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस को भी निकाला जा सकता है, और मुजरिम के परिवार के और लोगों को भी खतरनाक मानते हुए उनकी निगरानी की जा सकती है। मतलब यह होगा कि एक मुजरिम के परिवार के बेकसूर लोग भी पुलिस की गैरजरूरी और नाजायज निगरानी के घेरे में रहेंगे, और उनसे कोई गलती होने पर भी उसे गलत काम साबित करने की सहूलियत पुलिस के पास रहेगी, और ऐसे लोग दूसरे नागरिकों के मुकाबले कानूनी एजेंसी का खतरा अधिक झेलेंगे। जब सत्ता एक बड़े और व्यापक पूर्वाग्रह के साथ आज भी काम करते दिख रही है, तो नागरिकों की ऐसी प्रोफाइलिंग लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर देने का हथियार रहेगी। आज जो आधार कार्ड और दूसरे शिनाख्त-कागजात सरकार एक औजार की तरह पेश कर रही है, वे आज ही हथियार भी बनाए जा चुके हैं, और सरकारें उन्हें नापसंद लोगों के खिलाफ इस हथियार का इस्तेमाल कर सकती हैं, और कर रही हैं। इसे एक दूसरी बात से भी जोडक़र देखा जा सकता है कि पेगासस जैसे खुफिया घुसपैठिया साइबर-हथियार का इस्तेमाल पूरी आबादी के खिलाफ तो नहीं हो सकता इसलिए किन लोगों के खिलाफ इसे इस्तेमाल करना है वह लिस्ट तैयार करने में सरकार अपने बाकी पूर्वाग्रही जानकारी के साथ-साथ ऐसी प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल कर सकती है।
टेक्नालॉजी तो बहुत सारी बातों को मुमकिन कर रही है, लेकिन यह भी समझने की जरूरत है कि उसका इस्तेमाल कब उसे औजार से हथियार बना देता है, उसका अंदाज लगाए बिना, उसका अध्ययन किए बिना उसका इस्तेमाल शुरू ही नहीं करना चाहिए। लोगों को यह मिसाल भूलनी नहीं चाहिए कि अमरीकी वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन बम बनाने का एक औजार बनाया था, लेकिन उसे जापान के हिरोशिमा-नागासाकी के लोगों पर गिराना है यह फैसला तो अमरीकी सरकार ने उसे एक हथियार बनाकर लिया था। कुछ ऐसा ही हाल पेगासस से लेकर आधार कार्ड तक बहुत सी तकनीक का है, जिसे आतंकियों को पकडऩे से लेकर सरकारी काम की सहूलियत तक के नाम पर बनाया गया, लेकिन जो आज हथियार ही हथियार बनकर रह गई हैं। इसलिए जुर्म और मुजरिम की भविष्यवाणी करने वाले पुलिस के कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के खतरों को समझने की जरूरत अधिक है क्योंकि इससे इतनी अधिक निजी जानकारी कुछ उंगलियों पर आ जाती है, जिनमें से कुछ उंगलियां समाज के कुछ धर्मों, कुछ रंगों, कुछ जातियों का गला घोंटने के लिए बेताब रहती हैं। तकनीक के अंधाधुंध विकास को जायज ठहराने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन समाज वैज्ञानिकों को इनके खतरे सामने रखना चाहिए, और लोकतंत्रों में अदालतों को सरकार के तर्कों से परे भी कुछ समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। हिन्दुस्तान में तो संसद भी सरकार से पेगासस पर एक शब्द नहीं उगलवा पाई थी, यह तो सुप्रीम कोर्ट ही था जिसने हिन्दुस्तानी सरकार द्वारा अपने ही नागरिकों के खिलाफ इस घुसपैठिया फौजी सॉफ्टवेयर के हमले के आरोपों की जांच करवाना शुरू किया है। पुलिस की प्रोफाइलिंग के खतरे कम नहीं हैं, इस बात को लोगों को समझना चाहिए, और यह एक नए किस्म का टेक्नालॉजी आधारित रंगभेद रहेगा, या हिन्दुस्तान जैसे संदर्भ में यह एक नवसाम्प्रदायिकता रहेगी।
अपने आसपास बहुत से लोग हमें ऐसे देखने मिलते हैं जिन्हें अक्सर ही जिंदगी की किसी न किसी, या हर किसी, बात से शिकायत रहती है। नतीजा यह निकलता है कि उनके पास शिकायत, मलाल, या नाराजगी के अलावा आसपास के लोगों को देने के लिए और कुछ नहीं रहता। शायद ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखते हुए अभी दुनिया में एक जगह एक ऐसा महीना मनाया गया जिसमें हिस्सा लेने वाले लोगों के लिए यह शर्त रखी गई कि वे इस पूरे महीने को बिना कोई शिकायत किए हुए गुजारेंगे। ऐसी कोशिश करने वाले लोगों के पास मनोवैज्ञानिकों का यह निष्कर्ष था कि लोग जब शिकायत करते हैं तो उनका दिमाग स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है जो कि दिमाग के उन हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है जो परेशानी का इलाज ढूंढने का काम करते हैं।
इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करने वालों के पास यह वैज्ञानिक तथ्य भी है कि दिमाग के इस हिस्से को उस वक्त भी नुकसान पहुंचता है जब वे लगातार अनुपातहीन तरीके से दूसरों की शिकायत सुनते रहते हैं। इस विषय पर लिखी गई एक किताब में लेखक ने यह लिखा था कि शिकायतों से होने वाली परेशानी पैसिव स्मोकिंग जैसा नुकसान करती है जिसमें सिगरेट कोई और पी रहे हैं, लेकिन आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसे प्रयोग में शामिल होने वाले लोगों ने अपने तजुर्बे लिखे हैं जिन्हें पढऩा और सुनना दिलचस्प हो सकता है।
लोग अपने आसपास के लोगों से बहुत बुरी तरह प्रभावित होते हैं। बहुत से लोगों का यह मानना रहता है कि कोई व्यक्ति उतने ही अच्छे हो सकते हैं जितनी अच्छाई उनके आसपास के सबसे करीबी पांच लोगों की औसत अच्छाई होती है। सयाने बड़े बुजुर्ग हमेशा संगत के बारे में कहते आए हैं कि संगत अच्छी रखनी चाहिए। यह बात दुनिया की अलग-अलग संस्कृतियों और भाषाओं में अलग-अलग शब्दों में कही गई है, और चूंकि पुरूषवादी भाषा का हमेशा से बोलबाला रहा है इसलिए दार्शनिक बातें भी मानो महज पुरूषों के लिए कही जाती हैं, और कहा गया था- अ मैन इज नोन बाइ द कंपनी ही कीप्स। मतलब यह कि महिला तो अच्छी या बुरी तरह की संगत के लायक भी नहीं है, और महिला कैसे लोगों के साथ रहती है, या कैसे लोगों को साथ रखती है उससे भी कोई मायने नहीं रखता।
लेकिन आज के मुद्दे की बात पर लौटें, तो लोगों को बारीकी से यह सोचना चाहिए कि वे तमाम जिंदगी से और तमाम लोगों से अपनी शिकायतों को कम कैसे कर सकते हैं? जिस तरह एक गिलास में आधे भरे पानी को देखकर आधी खाली ग्लास पर अफसोस भी किया जा सकता है, और आधे भरे पानी की खुशी भी मनाई जा सकती है, उसी तरह असल जिंदगी भी रहती है। लोग अंबानी की दौलत से अपनी तुलना करें, तो नवीन जिंदल भी बाकी पूरी जिंदगी मलाल मनाते काट सकता है, और नहीं तो जिनका पैर टूट गया है वे भी यह देखते हुए तसल्ली से जी सकते हैं कि जिन लोगों के दोनों पैर कट चुके हैं वे लोग भी जिंदा रहते हैं, और नकली पांवों के साथ एवरेस्ट भी जीतकर आ जाते हैं।
लोगों को दुनिया में नकारात्मकता कम करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए और स्थायी रूप से चौबीसों घंटे मलाल का गमी का जलसा मनाना बंद करना चाहिए। ऐसा करने पर लोगों को यह समझ में आएगा कि जिंदगी की बहुत सी तकलीफें तो अपनी ही सोच से पैदा होती है, और अपनी कुछ तकलीफों के बारे में पूरे वक्त सोचने और लोगों से बार-बार कहने की वजह से उन तकलीफों की गूंज अपने ही दिल-दिमाग में भर जाती हैं, और कई गुना अधिक तकलीफ देती हैं। अपनी जिंदगी से हताश-निराश लोग मानो दुनिया की शिकायत करते हुए अपने ही बारे में इतना बुरा बोलने लगते हैं कि धीरे-धीरे उनके शब्द उन पर ही खरे उतरकर यह साबित करने लगते हैं कि अगर यही बात उन्हें इतनी पसंद है, तो फिर यही सही। वैसे भी किसी समझदार इंसान ने कभी कहा था कि अपने खुद के बारे में भी कभी बहुत बुरा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बंद घड़ी का बताया वक्त भी हर दिन दो बार तो सही निकलता ही है।
फिर यह बात भी समझना चाहिए कि शिकायतों से लिपटे हुए जीने वाले लोगों से आसपास के समझदार लोग भी थककर कतराने लगते हैं। सिर्फ वे ही लापरवाह लोग आसपास रह जाते हैं जिन्हें इस नकारात्मकता से खुद को होने वाले नुकसान की फिक्र नहीं रहती। जबकि संक्रामक रोग की तरह शिकायती जिंदगी लगातार लोगों को और शिकायतों का अहसास कराती चलती है, और यह सिलसिला अपने भीतर भी बढ़ते चलता है, और अपने इर्द-गिर्द भी। इसलिए समझदार लोगों को शिकायतों के इस जाल में फंसने से बचना चाहिए, चाहे यह खुद की कही जा रही शिकायतें हों, या कि दूसरों से सुनी गई शिकायतें हों। शिकायतों को सुनना भी तभी चाहिए जब किसी सरकारी या निजी नौकरी के तहत शिकायतों को सुनने और दर्ज करने के लिए तनख्वाह मिलती हो। जब तक रोजी-रोटी न जुड़ी हो, लोगों को लगातार शिकायतें सुनने से भी मना कर देना चाहिए क्योंकि हर शिकायत का इलाज तो उस कथित ईश्वर के पास भी नहीं है जिसे कि सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहा जाता है।
कुल मिलाकर एक महीना ऐसा गुजारकर देखें जिसमें जिंदगी से, लोगों से, दुनिया से कोई शिकायत न रहे, और हो सकता है कि महीना गुजरने तक आपको यह अहसास होने लगे कि आप एक बेहतर दुनिया में, बेहतर लोगों के बीच, एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
जो चीन दशकों से एक बच्चे की नीति पर चल रहा था और वहां के शादीशुदा जोड़ों को दूसरा बच्चा पैदा करने की इजाजत नहीं थी, उसने अभी 2016 में ही दूसरे बच्चे की इजाजत दी थी और 5 बरस के भीतर आज नौबत यह आ गई है कि वहां के सरकारी मीडिया ने एक सम्पादकीय लिखा है कि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को तीसरा बच्चा पैदा करना ही होगा, और एक या दो बच्चे रखने का कोई बहाना नहीं चलेगा। सरकार ने अभी-अभी वहां पर आबादी बढ़ाने के लिए तीसरे बच्चे पर कई तरह की टैक्स छूट और सब्सिडी की घोषणा भी की है। लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि वे कम से कम 3 बच्चे तो पैदा करें। जिस चीन में कई दशक से सरकार एक बच्चे की नीति को पूरी ताकत से लागू किए हुए थी, वह अब तीन बच्चों के लिए बढ़ावा देने की नौबत में आ गई है क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था में, वहां की आबादी बड़ा योगदान दे रही है, और सरकार को यह लगता है कि अगर आबादी गिरती चली जाएगी तो चीन की अर्थव्यवस्था को संभालना भी मुश्किल होगा। आज वहां पर लोगों की दिलचस्पी अधिक बच्चे पैदा करने में नहीं रह गई है, और दुनिया भर के जनसंख्या विशेषज्ञों में यह माना जाता है कि एक जोड़े के दो बच्चे अगर होते चलें तो ही देश की आबादी उतनी बनी रह सकती है।
दूसरी तरफ हिंदुस्तान में आबादी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस देश में सत्ता और राजनीति से जुड़े हुए, अर्थव्यवस्था जुड़े हुए बहुत से लोग यह मानते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी बहुत बड़ी समस्या है, और आबादी घटाए बिना यहां का काम नहीं चलेगा। इस जगह हमने बरसों से यह बात बार-बार लिखी है कि आबादी किसी देश के लिए बोझ तभी बनती है जब वहां की सत्ता उस आबादी के उत्पादक उपयोग की योजनाएं नहीं बना पाती। वरना एक इंसान, और खासकर मजदूर दर्जे के गरीब इंसान जितनी खपत करते हैं, उससे अधिक पैदा करते हैं। उन्हें जमीन पर खेती करने मिल जाए तो भी वह साल भर में जितना खाते हैं, उससे अधिक उगाते हैं। वे शहरों में, कारखानों में, कंस्ट्रक्शन में, मेहनत करते हैं तो भी वे अपने खाने से अधिक उत्पादकता देश की अर्थव्यवस्था में जोड़ते हैं। इसलिए आबादी को जो लोग बोझ मानते हैं वे इस बात को अनदेखा करते हैं कि वहां देश प्रदेश की सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, और ऐसी योजनाएं नहीं बनाई हैं कि लोगों को रोजगार मिले, लोग काम कर सकें, और उनकी उत्पादकता राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जुड़ सके।
मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ में लोग गोबर बेचकर भी कुछ कमा रहे हैं, और गोबर का खाद बनाकर भी। लेकिन देशभर में जो काम बड़े पैमाने पर होना चाहिए वह ग्रामीण रोजगार और स्वरोजगार का है जिसके तहत तरह-तरह के पशु-पक्षी पालना, शहद और रेशम का काम करना, लाख की खेती करना, मशरूम उगाना, खेतों की उपज को मशीनों से प्रोसेस करके उन्हें बड़े शहरों के कारखानों तक भेजना, कपड़े बुनना, दोना-पत्तल बनाना, जैसे कई हजार किस्म के काम हो सकते हैं जो अलग-अलग इलाकों में वहां के जंगलों, खेतों और वहां की तरह-तरह की उपज के आधार पर तय हो सकते हैं। ऐसे कोई भी काम करने वाले लोग किसी भी तरह से उस देश पर बोझ नहीं हो सकते। देश पर बोझ तो दरअसल सत्ता पर बैठे हुए वे लोग हैं जो कि लोगों को स्वरोजगार देने की योजना बनाने की क्षमता नहीं रखते, लेकिन सत्ता पर आ जाते हैं, और वहां बने रहते हैं।
भारत और बांग्लादेश अभी पौन सदी पहले तक एक ही देश थे। फिर वह हिस्सा पाकिस्तान बना, और बाद में भारत के बनवाए हुए बांग्लादेश बना। उसने राजनीतिक अस्थिरता, फौजी हुकूमत, और हिंसा का बहुत लंबा दौर देखा। बाढ़ का बहुत बड़ा नुकसान झेला। उसका विकास हिंदुस्तान के मुकाबले बहुत पीछे होना चाहिए था। लेकिन गरीबी, धार्मिक कट्टरता, अशिक्षा, और राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद बांग्लादेश आज सकल राष्ट्रीय उत्पादन में भारत के आगे निकल गया है। दुनिया के खेल-कूद और फैशन के कोई ऐसे बड़े ब्रांड नहीं हैं, जिनके कपड़े और जूते, फुटबॉल और दूसरे सामान बांग्लादेश में ना बनते हों। वहां की आम आबादी ने बड़ी-बड़ी महंगी और आयातित मशीनों पर तरह-तरह की सिलाई करना सीख लिया है और बांग्लादेश पूरी दुनिया के लिए एक दर्जी की तरह काम कर रहा है। उसने अपनी अर्थव्यवस्था को भारत की प्रति व्यक्ति की अर्थव्यवस्था के भी ऊपर पहुंचा दिया है। अब इस बात में, इस काम में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हिंदुस्तानी नहीं कर सकते थे? यह देश तो बड़े-बड़े शैक्षणिक संस्थानों का देश है, आईआईटी और आईआईएम का देश है जहां से निकले हुए लोग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हांक रहे हैं। ऐसे लोग तैयार करने वाला यह देश अपने मामूली मजदूरों को सिलाई का वह काम भी नहीं सिखा पाया जिसके चलते बांग्लादेश विदेशी मुद्रा कमाने वाला छोटा सा, लेकिन बड़ा देश हो गया है। अब यह तो देशों की सरकारों पर रहता है कि वे अपने लोगों को कितना उत्पादक बना सकती हैं। बांग्लादेश की तरह अपने लोगों को हुनर सिखाकर, उनके लिए रोजगार जुटाकर, उनके लिए मशीनें लगाकर, दुनिया भर का कारोबार लाकर जो सरकार इस ट्रेन को पटरी पर दौड़ा सकती है, उसे फिर आगे फिक्र करने की जरूरत नहीं रहती कि उसकी आबादी बढ़ रही है। बांग्लादेश में इस तरह का रोजगार करने वाले लोग हिंदुस्तान के आम लोगों के मुकाबले बहुत अधिक कमाई कर रहे हैं और उनके हुनर में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे हिंदुस्तानी नहीं सीख सकते थे। हिंदुस्तानी बाजार में बिक रहे सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय फैशन ब्रांड देखें, तो उनके भीतर लेबल लगा दिखता है, बांग्लादेश, वियतनाम और दूसरे छोटे-छोटे देशों में उनके बनने का। यह काम हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता था?
इसलिए जिस तरह आज चीन अपनी आबादी बढ़ाने पर आमादा है और वहां के लोग अधिक बच्चों का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन देश की सरकार लगी हुई है कि लोग कम से कम 3 बच्चे तो पैदा करें ही। आज हिंदुस्तान में बच्चे कम पैदा करने की जो मुहिम चल रही है और हर बात के लिए जिस तरह अधिक आबादी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है उस सोच को सुधारने की जरूरत है। आबादी को हुनर सिखाकर, काम से लगाकर, इस देश की अर्थव्यवस्था को आसमान पर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन जब सरकारों की दिलचस्पी बड़े-बड़े कारखानों तक सीमित रह जाती है और आम जनता को स्वरोजगार के काम मुहैया कराने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती, तो वैसे ही देश में आबादी बोझ हो सकती है। चीन में आज इतना काम है, और बाकी दुनिया से जुटाया हुआ इतना काम है कि एक-एक कारखाना कामगार को ओवरटाइम करना पड़ता है, उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिल पाती है। हम उनके काम के हालात या उनके मानवाधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पास काम कितना है इसकी बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां के कारखानेदार, और वहां की सरकार, इन दोनों को वहां के कामगार से ओवरटाइम करवाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान महज सपना देखते बैठा है कि वह चीन से बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा और इस सपने को पूरा करने के लिए उसके पास जमीन पर कोई कोशिश नहीं है। जब तक किसी देश की राष्ट्रीय उत्पादकता गिनी-चुनी कंपनियों तक सीमित रहेगी और आम जनता की उत्पादकता का उसमें योगदान बढ़ाने की फिक्र नहीं की जाएगी तब तक ही आबादी बोझ बनी रहेगी। वरना कुदरत ने इंसानों को ऐसा बनाया है कि वे अपनी जरूरत से बहुत अधिक पैदा करने के लायक हैं। हिंदुस्तान और चीन के मॉडल सामने रखकर समझने की जरूरत है, और हिंदुस्तान और बांग्लादेश की तुलना करके भी हिंदुस्तान कुछ सीख सकता है। आबादी अधिक होने से देश पर पडऩे वाले बोझ का रोना फिजूल की बात है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से भेजे गए एडवोकेट केटीएस तुलसी ने कल बिलासपुर में एक व्याख्यान में कई बड़े दिलचस्प तथ्य रखे। हिंदुस्तान में यह तो माना जाता है कि अदालतें बहुत धीमी रफ्तार से काम करती हैं, लोगों को फैसला पाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है इसकी एक बड़ी वजह एडवोकेट तुलसी ने कल अपने व्याख्यान में बताई। उन्होंने कहा कि कई देशों में जैसे ही थानों में किसी जुर्म की या हादसे की जानकारी के लिए फोन जाता है तो वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, और उसी को एफआईआर माना जाता है। भारत में भी एफआईआर का हिंदी प्रथम सूचना रिपोर्ट होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन होता नहीं है कई बार तो एफआईआर लिखने के लिए महीनों तक लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं, और पुलिस के बारे में कहा जाता है कि वह आमतौर पर एफआईआर लिखने के लिए उगाही भी कर लेती है।
एडवोकेट तुलसी ने बताया कि दुनिया के बेहतर इंतजाम वाले देशों में टेलीफोन पर मिली शिकायत या जानकारी को कई थानों के लोग सुनते हैं, तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, पुलिस के साथ ही फॉरेंसिक मोबाइल टीम भी चली जाती है और आधे घंटे में ही फिंगरप्रिंट बगैर इक_े कर लिए जाते हैं। इन सबके चलते हुए सुबूत विश्वसनीय रहते हैं, मददगार रहते हैं, और अदालती सुनवाई और फैसलों में देर नहीं लगती। हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने बताया कि यहां पर छोटे अपराधों में चालान पेश करने के लिए 60 दिन और बड़े मामलों में 90 दिन का समय मिलता है लेकिन अक्सर इतने वक्त में भी चालान पेश नहीं होते, नतीजा यह होता है कि भारत सजा दिलवाने का प्रतिशत सिर्फ 2.9 है जबकि कई देशों में यह 48 फीसदी या उससे अधिक है। उन्होंने कहा कि यहां एक-एक मजिस्ट्रेट या जज के पास हर दिन करीब 60 मामले आते हैं, और किसी के लिए यह मुमकिन नहीं होता कि 60 अलग-अलग मामलों की फाइलों को देखकर पढ़ सकें, इसलिए एक केस में सिर्फ दो-तीन मिनट का समय मिलता है। नतीजा यह है कि जेलों में भी भयानक भीड़ है, जहां 80 फीसदी विचाराधीन कैदी हैं, और सुनवाई में देरी के कारण उन्हें एक निश्चित समय सीमा में जमानत का फायदा भी नहीं मिलता।
अभी जब हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक सही या गलत मामले में गिरफ्तार किया गया तो उसकी जमानत के लिए मानो धरती और आसमान को एक कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सबसे दिग्गज और शायद हिंदुस्तान के सबसे महंगे वकीलों में से एक को लाकर खड़ा कर दिया गया जिसने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के केस की धज्जियां उड़ा दीं। केस को इतना कमजोर साबित कर दिया कि जज को कहना पड़ा कि आर्यन के खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत नहीं दिख रहा है. और यह मामला उस अफसर के बनाए केस का है जो बड़ा नामी-गिरामी है, और जिसने हिंदुस्तान के ऐसे बहुत बड़े-बड़े फिल्म कलाकारों को नशे के मामलों में घेरा हुआ है। उसका बनाया हुआ केस इतना कमजोर साबित हुआ कि न सिर्फ हाई कोर्ट ने जमानत दी बल्कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्यवाही की धज्जियां भी उड़ा दीं। अब सवाल यह है कि यह केस सच्चा था या गढ़ा हुआ था, जो भी था, यह इतना कमजोर बना था कि यह जमानत के स्तर पर भी नहीं टिक पाया, जमानत की सुनवाई में ही इसकी बुनियादी कमजोरियां उजागर हो गईं। दूसरी तरफ पुलिस के आम मामलों में हाल यह रहता है कि पुलिस सच्चे गवाहों के साथ-साथ कुछ पेशेवर गवाहों को भी मामले में जोड़ देती है क्योंकि उसका यह मानना रहता है कि सच्चे गवाह अदालत में मुजरिम के वकील के सवालों के सामने टिक नहीं पाते, लडख़ड़ा जाते हैं, और वैसे में घिसे और मंजे हुए पेशेवर गवाह ही पुलिस के मामले को साबित कर पाते हैं। अब यह कैसी न्याय व्यवस्था है जिसकी शुरुआत ही झूठ से और फरेब से होती और जिससे इंसाफ की उम्मीद की जाती है?
दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जेलों की हालत को देखें तो वहां बहुत अमानवीय हालत में लोग फंसे हुए हैं, उन्हें अदालतों में पेश करने के लिए पुलिस कम पड़ती है, और पुलिस बार-बार अदालत से अगली पेशी मांगती है कि पुलिस बल की कमी है। एक दूसरी बात जिसे समझने की जरूरत है, जेल और अदालत, इनका एक-दूसरे से इतने दूर रहना भी ठीक नहीं है। फिर जो पुलिस जुर्म की जांच करती है, उस पुलिस के जिम्मे सौ किस्म के दूसरे काम डालना भी ठीक नहीं है। इसके लिए विदेश को देखने की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में ही कुछ प्रदेशों में जुर्म की जांच का काम पुलिस के अलग लोगों के हवाले रहता है, और कानून-व्यवस्था को कायम रखने का काम दूसरे पुलिसवालों के हवाले रहता है। वरना होता यह है कि थाने के इलाके में कोई मंत्री, मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं तो वहां की पुलिस पूरे-पूरे एक-दो दिन उसी इंतजाम में लग जाती है, और उसकी तमाम किस्म की जांच धरी रह जाती है। वैसे दिनों पर पुलिस अदालत में भी सुबूत या डायरी लेकर पेश नहीं हो पाती, सरकारी वकील के पास नहीं जा पाती। इन सबको देखते हुए पुलिस के दो हिस्से साफ-साफ बना देना जरूरी है, एक हिस्सा जिसे जुर्म की जांच करना है, उसे किसी भी किस्म के दूसरे काम से अलग रखना चाहिए। भारत में जहां-जहां ऐसा बंटवारा कर दिया गया है वहां पर जुर्म की बेहतर जांच होती है। वरना थानों की पुलिस के हवाले जब जांच रहती है तो जब वहां कोई धरना प्रदर्शन नहीं रहता, जब वहां कोई जुलूस नहीं निकलते रहता, जब वहां कोई धार्मिक त्यौहार नहीं मनाया जाता, जब वहां किसी मंत्री या नेता का दौरा नहीं रहता, तब पुलिस कभी-कभी जांच भी कर लेती है। यह सिलसिला खत्म होना चाहिए।
एडवोकेट तुलसी ने जो बात की है उसका एक और पहलू या तो उनके भाषण में नहीं आया है या भाषण की खबर में नहीं आया है। हिंदुस्तान में हाल के बरसों में बहुत सी जांच एजेंसियां लोगों को घेर कर रखती हैं, और उन पर ऐसे कड़े कानून लगाती हैं कि उनकी जमानत ना हो सके। इसके बाद उनकी जमानत को रोकने के लिए ही पूरा दमखम लगा देती हैं। भीमा कोरेगांव का केस हो या शाहीन बाग का केस हो, या दिल्ली के किसी दूसरे प्रदर्शन का केस हो, जहां कहीं भी लोगों को निशाने पर लेकर उन्हें प्रताडि़त करने की सरकार की नीयत रहती है, वहां जांच एजेंसियां उन्हें जमानत ना मिलने देकर तरह-तरह से प्रताडि़त करती हैं, और मामले की सुनवाई भी शुरू नहीं हो पाती और लोगों के कई बरस कैद में निकल जाते हैं।
छत्तीसगढ़ के जिस बिलासपुर हाईकोर्ट के वकीलों के बीच एडवोकेट तुलसी का यह व्याख्यान हुआ है वहीं पर वकालत करने वाली सुधा भारद्वाज को भीमा कोरेगांव केस में बंद हुए बरसों हो रहे हैं, और सरकारी एजेंसी उनकी जमानत नहीं होने दे रही। अब इतने बरसों की कैद के बाद अगर वे बेकसूर भी साबित हो जाती हैं, तो भी क्या होगा?सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्र नेताओं, पत्रकारों का एक अलग ऐसा तबका है जो कि सरकार से अपनी असहमति की वजह से उसके निशाने पर रहता है और सरकार की एजेंसियां जिनके खिलाफ ऐसे कड़े कानून के तहत केस दर्ज करती हैं कि उनकी जमानत ना हो सके।
अब हिंदुस्तान के भीतर राजद्रोह और देशद्रोह के मामले बड़ी आसानी से लोगों के खिलाफ दर्ज कर दिए जा रहे हैं, लेकिन बरसों के बाद जाकर अदालत को समझ आता है कि इस मामले में कोई सुबूत नहीं है, कोई दम नहीं है, और तब जाकर लोगों की जमानत हो पाती है। अभी जब यह लिखा ही जा रहा है उसी वक्त यह खबर आई है कि जेएनयू के एक पूर्व छात्र और शाहीन बाग में सीएए-एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले शरजील इमाम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कल जमानत मिली है। वे साल भर से गिरफ्तार करके जेल में रखे गए थे और उन पर यह आरोप था कि उन्होंने उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत के बाकी हिस्सों से अलग होने के लिए उकसाया। इस मामले में शरजील के खिलाफ मणिपुर, असम, और अरुणाचल की पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की थी, और असम, और अरुणाचल के मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। फिलहाल यह छात्र नेता दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, और उस पर देशद्रोह के आरोप लगाए गए हैं।
अब एडवोकेट तुलसी ने जिन मामलों की भीड़ के बारे में कहा है उससे परे यह अलग किस्म का रुझान हाल के वर्षों में हिंदुस्तान में सामने आया है जब लोगों की जमानत रोककर लंबे समय तक कैद में रखा जाता है, और उसे कैद कहा भी नहीं जाता। यह सिलसिला भी खत्म होना चाहिए क्योंकि इससे भी जेलों में भीड़ बढ़ रही है, अदालतों में मामले बढ़ रहे हैं, पुलिस और जांच एजेंसियों पर बोझ बढ़ रहा है, और लोगों का जमानत पाने का जायज हक छीना जा रहा है। इस किस्म की बहुत सी बातों पर सुप्रीम कोर्ट को भी गौर करना चाहिए। क्योंकि ऐसा किसी एक मामले में ही हो रहा हो ऐसा नहीं है, यह देश भर में केंद्र और राज्य सरकारों की तरह-तरह की एजेंसियां सत्ता को नापसंद लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कर रही हैं, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। देखते हैं कि एडवोकेट तुलसी की छेड़ी गई बात कहां तक आगे बढ़ती है।
हाल के महीनों में हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से ऐसे फैसले दिए हैं जिनसे केंद्र और राज्य सरकारों को झटका लगा है, और जिनसे नागरिक स्वतंत्रता का हक दमदारी से फिर से कायम होते दिख रहा है। लेकिन कभी-कभी बहुत तकनीकी आधार पर दो बड़ी अदालतों के बीच में इस तरह का टकराव होता है कि उसमें नीचे की अदालत का रुख अधिक सकारात्मक दिखता है, और सुप्रीम कोर्ट उसे एक तकनीकी आधार पर पलट देता है। ऐसा ही एक मामला अभी कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले को लेकर आया जिसने राज्य में मनाए जाने वाले काली पूजा, दिवाली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस, और नए साल के त्योहारों पर पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही पटाखों के उपयोग को प्रतिबंधों के साथ छूट दे चुका है, और पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 1 नवंबर को आया था और उसके तुरंत बाद आई दिवाली पर दिल्ली की हवा में इतना जहर घुल गया है कि आज दिवाली के तीसरे दिन भी दिल्ली में सांस लेना महफूज नहीं है।
देश की सबसे बड़ी पर्यावरण संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की एक रिपोर्ट कहती है कि ‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ओर से पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 और पीएम 10 के स्तर की 24 घंटे निगरानी करने वाले केंद्रीय नियंत्रण कक्ष (सीसीआर) ने 5 नवंबर, 2021 की रात 9.30 बजे के बाद अपडेट देना बंद कर दिया है। दीवाली की रात से 5 नवंबर के रात 9.30 बजे तक यानी कुल 32 घंटे तक पीएम 2.5 हवा में आपात स्तर (300 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) पर ही बना रहा।’ सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि प्रदूषण का स्तर एक सीमा से अधिक बढऩे पर एक आपात योजना लागू की जाए जिसके तहत कई किस्मों के काम दिल्ली में बंद कर दिए जाएं। लेकिन एक तरफ दिल्ली के आसपास खेतों में फसलों के ठूंठ जलाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ पटाखे इतनी बड़ी संख्या में छोड़े गए कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किसी ने भी नहीं माना।
कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश बिल्कुल इसी बात को सोचते हुए दिया गया था कि पटाखों और ग्रीन पटाखों में फर्क कर पाना प्रशासन के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि पटाखा बनाने वाले लोग उन पर ग्रीन पटाखे का लेबल लगाकर बेच रहे हैं, और सरकारी अधिकारी कर्मचारी इसकी कोई शिनाख्त नहीं कर सकते। हकीकत भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट की नजरों के सामने, सुप्रीम कोर्ट के जजों के फेफड़ों को प्रभावित करते हुए दिल्ली के इलाके में दिवाली पर जितने पटाखे फोड़े गए, उन पर अदालत का, या सरकार का कोई भी जोर नहीं चला। बहुत सी बातें ऐसी रहती हैं जिनको एक फैसले में तो लिखा जा सकता है, लेकिन इन पर अमल का कोई जरिया नहीं रहता। करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में थाने के स्तर तक के पुलिस अफसर की शिनाख्त कर दी थी कि जिस इलाके में 2 घंटे के बाद पटाखे फोड़े जाएंगे या प्रतिबंधित पटाखे फोड़े जाएंगे उन इलाकों के थाना प्रभारी भी जिम्मेदार रहेंगे, लेकिन उस बात का क्या हुआ? न तो कहीं पर शासन-प्रशासन ने इस बात को दर्ज किया, न ही कोई केस दर्ज हुआ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तकनीकी आधार पर हाईकोर्ट के आदेश को खारिज तो कर दिया कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देश में प्रदूषण की खतरनाक हालत को जरा भी ध्यान में नहीं रखा, जिसे सोचते हुए, यह जिसका हवाला देते हुए, उसने खुद पहले एक लंबा चौड़ा आदेश जारी किया था।
हम पिछले दस दिनों में दो बार इस मुद्दे पर इसी जगह पर लिख चुके हैं, और फिर लिखने की बात इसलिए महसूस कर रहे हैं कि दिवाली के बाद भी जिस तरह दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एकदम जहरीला बना हुआ है, और उसमें पटाखों का जितना बड़ा योगदान रहा है उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को अगले साल के लिए अभी से आदेश जारी करना चाहिए ताकि पटाखा उद्योग और कारोबारी अगले साल फिर यह रोना न रोएं कि उनका धंधा प्रभावित होगा। अदालत को यह भी देखना चाहिए कि जिस पुलिस के भरोसे वह बहुत से आदेशों को जारी करने की सोचती है क्या उस पुलिस के पास सचमुच ऐसा कोई खली वक्त है कि वह आबादी के बड़े हिस्से से टकराव मोल ले, दिवाली मना रहे लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज करे, उसके सुबूत रिकॉर्ड करे, और उन्हें अदालतों में साबित करे? न पुलिस के पास इतना वक्त है, और न अदालतों के पास. इन दोनों के जिम्मे पहले से जितना बोझ पड़ा हुआ है वह उसी से नहीं निपट पा रहे हैं, पुलिस अधिकतर मामलों की समय पर जांच नहीं कर पाती, और अदालत से तो शायद ही किसी मामले का समय पर निपटारा हो सकता है। तो ऐसी हालत में ऐसे अमूर्त किस्म के (अनइन्फोरसिएबल), आदेश या फैसले सुप्रीम कोर्ट को या किसी दूसरी अदालत को नहीं देने चाहिए, जिन पर अमल नहीं हो सकता।
देश की हकीकत यह है कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के देखते हुए भी लोगों की भीड़ ने जब बाबरी मस्जिद गिरा दी थी तब भी यही तर्क सामने आया था कि अगर इतनी भीड़ पर पुलिस कार्यवाही की गई होती तो सैकड़ों लोग मारे गए होते। इसलिए जो कुछ हो सकता था वह समय के पहले ही हो सकता था। पटाखों को लेकर जो प्रतिबंध लागू हो सकते हैं वे दिवाली के काफी पहले से ही लागू किए जा सकते हैं वह उनके बनाने और बिकने पर ही लागू किए जा सकते हैं एक बार लोगों के घर अगर पटाखे पहुंच गए तो उसके बाद कोई प्रतिबंध लागू नहीं हो सकते। हिंदुस्तान की कोई पुलिस अपने शहर की आबादी के एक बड़े हिस्से से टकराव नहीं ले सकती। एक-एक पुलिस सिपाही क्या पटाखे जला रहे सैकड़ों लोगों को किसी भी तरह से रोक सकते हैं ?
फिर सुप्रीम कोर्ट की इस सोच में भी हमको एक खामी दिखती है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। आज जब ब्रिटेन में ग्लास्गो शहर में दुनिया भर से 20,000 से अधिक लोग इकट्ठे होकर पर्यावरण को बचाने की बात सोच रहे हैं, और लगातार यह फि़क्र की जा रही है कि धरती को कैसे बचाया जाए, कैसे प्रदूषण को कम किया जाए, कैसे मौसम की मार को बढऩे से रोका जाए, तो ऐसे में अगर हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट पटाखों पर रोक को लेकर एक दकियानूसी और परंपरागत सोच को आगे बढ़ाता है कि पटाखों पर पूरी रोक नहीं लगाई जा सकती, तो उसकी यह सोच गलत है। जिस सामान से केवल हवा प्रदूषित हो, हवा में असहनीय शोर गूंजे, उसमें जहर फैले, उसे जलाने या फोडऩे का हक किसी को कैसे दिया जा सकता है? जब हिंदुस्तान में पटाखों का इस्तेमाल शुरू हुआ था तब लोकतंत्र नहीं था, और उस वक्त कोई ऐसे कानून नहीं थे कि वे दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले सामानों पर रोक लगाएं। लेकिन वक्त के साथ-साथ ऐसे नुकसान को नापने के वैज्ञानिक पैमाने सामने आए. आज प्रदूषण को नापने के ठोस तरीके मौजूद हैं।
आज यह तक मौजूद है कि किस तरह प्रदूषण के चलते हुए अकेले दिल्ली शहर में पिछले 1 बरस में कितने हजार अतिरिक्त लोगों की मौत हुई है. तो ऐसे में पटाखों पर पूरी रोक क्यों न लगाई जाए? किसी के अपनी खुशी मनाने के ऐसे जहरीले तरीके को दूसरों की सेहत को बर्बाद करने की छूट क्यों दी जाए? और फिर पटाखे कौन सी धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं? धार्मिक परंपरा तो तालाबों और नदियों में मूर्तियों के विसर्जन करने की भी रही है, जिन पर हाल के वर्षों में अदालतों ने और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तरह-तरह की रोक लगाई ही है। नदियों में जिस तरह से अंतिम संस्कार का काम होता था, उस पर कानून ने रोक लगाई ही है। इसलिए वक्त को देखते हुए, आज की हिंदुस्तानी आबादी की सेहत को देखते हुए, पटाखों पर पूरी की पूरी रोक लगानी चाहिए, और यह रोक अभी समय रहते लगा देनी चाहिए ताकि कुछ महीने बाद पटाखा निर्माता या कारोबारी आकर अदालत में खड़े ना हो जाए कि उनके बनाए हुए पटाखों का क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट को इस हकीकत को याद रखना होगा कि देश में पटाखों का सबसे बड़ा इस्तेमाल साल में एक-दो दिनों के कुछ घंटों में ही होता है और यही सबसे घने प्रदूषण की वजह है, लेकिन बाकी वक्त भी जब पटाखे फोड़े जाते हैं तो उस वक्त अंधाधुंध शोर होता है, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, और बीमारों से लेकर सोए हुए लोगों तक को भारी तकलीफ होती है, फायदा किसी का भी नहीं होता है। किसी को भी अपनी खुशी मनाने के लिए ऐसे हिंसक तरीकों को इस्तेमाल करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए जो कि सौ-पचास बरस पहले की हल्की आबादी में तो चल जाते थे, लेकिन आज जब चारों तरफ इमारतें हैं, तब उनके बीच में ये पटाखे अधिक शोर करते हैं, अधिक नुकसान करते हैं।
कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला एकदम ही सही था, वह शासन प्रशासन के ऊपर से एक अनावश्यक सार्वजनिक दबाव को भी घटाने वाला था, और अगर सुप्रीम कोर्ट अपने कमरे में बैठकर यह सोचता है कि उसके फैसले को लागू करवाने की पूरी ताकत शासन-प्रशासन में है तो बहुत से फैसलों पर यह बात लागू नहीं होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। पर्यावरण के नुकसान रोकने के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उन्हें अदालत तक जाकर फिर से पिटीशन लगाना चाहिए और अगले बरस के लिए, अगले बरस तक के लिए, और उसके बाद के लिए, एक ऐसा आदेश पाने की कोशिश करनी चाहिए जो देश में पटाखों को पूरी तरह से बंद करे।
अगर खुशी मनाने का यही एक तरीका रह गया है तो यह तरीका आज हिंसक साबित हो चुका है. जहां तक धार्मिक परंपराओं की बात है तो कई बरस पहले इस देश में सती प्रथा को भी धार्मिक माना जाता था, और बाल विवाह को भी धार्मिक माना जाता था, देवदासी भी धार्मिक थी, और तीन तलाक भी धार्मिक था। लेकिन वक्त के साथ-साथ इन सभी में बदलाव किया गया, नए कानून बने, कई अदालतों ने फैसले दिए, तो कहीं सरकार ने संसद से, और विधानसभाओं से कानून बनवाए, और धार्मिक व सार्वजनिक मनमानी को खत्म किया। इसलिए परंपरा का नाम लेकर हिंसा को जारी नहीं रखा जाना चाहिए, और कोलकाता हाई कोर्ट का एकदम सही फैसला पूरे देश में लागू होना चाहिए, और क्योंकि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है, और वह खुद ही देख चुका है कि एक हफ्ते के भीतर ही किस तरह उसके फैसले को हर गली-मोहल्ले में फाडक़र फेंक दिया गया, इसलिए अब उसे एक ऐसा फैसला देना चाहिए जिस पर अमल हो सके। अभी से यह फैसला आने से देश का संगठित और असंगठित पटाखा उद्योग अपने आपको संभाल सकेगा और केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे काम में लगे हुए लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार तुरंत ही उपलब्ध कराना चाहिए जिसके लिए सरकारों के पास दर्जनों योजनाएं हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा आज बड़े निराश होंगे। कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेटिकन जाकर पोप से मुलाकात की तस्वीरें चारों तरफ छाई हुई हैं, और खुद प्रधानमंत्री के ट्विटर और फेसबुक जैसे पेज लगातार इन तस्वीरों को पोस्ट कर रहे हैं। वे पोप से गले मिल रहे हैं, उनके गाल से गाल सटा रहे हैं, और बाइबल को उठाकर सिर पर रख रहे हैं। यह एक अलग बात है कि हिंदुस्तान में गोवा में चुनाव होने जा रहे हैं जहां ईसाई बहुतायत है, लेकिन रामेश्वर शर्मा को इस वजह से भी राहत मिलने वाली नहीं है। अभी कुछ ही समय तो हुआ है जब उन्होंने एक कार्यक्रम में वीडियो कैमरे के सामने कहा था कि हिंदुओं को फादर और चादर से दूर रहना चाहिए। फादर तो जाहिर है ईसाई के लिए कहा जाता है, और चादर जाहिर है कि मुस्लिम महिलाओं के ओढ़ने के कपड़े को कहा जाता है। उन्होंने दशहरा के कार्यक्रम में मंच से भाषण देते हुए कहा था कि फादर और चादर तुम्हें बर्बाद कर देंगे, यह पीर बाबा तुम्हारे मंदिर जाने में बाधा हैं, पीरों को पूजने वालों को कह दो कि तुम जमीन में दफन करने में भरोसा रखते हो, और हम दुनिया को जलाने वालों पर भरोसा रखते हैं, जो बजरंगबली हैं. इस तरह की बहुत सी बातें वह हिंदुत्व को लेकर अपनी हमलावर सोच के तहत करते रहते हैं, इसलिए उनका यह हक भी बनता है कि पोप से इस तरह गले मिलते, लिपटते नरेंद्र मोदी को देखकर वह निराश हो जाएं।
लेकिन ऐसे विधायक की ऐसी बातों को छोड़ भी दें तो भी लोगों का धर्म से जुड़े लोगों के बारे में तजुर्बा बड़ा गड़बड़ रहता है। अभी जाने-माने फिल्म निर्देशक प्रकाश झा की एक वेब सीरीज 'आश्रम' की शूटिंग के दौरान मध्यप्रदेश में बजरंग दल ने प्रकाश झा पर हमला किया, क्योंकि यह वेब सीरीज 'आश्रम' नाम वाली है, और इसमें किसी बाबा के कुकर्मों का जिक्र है। जब इस हमले की खबर चारों तरफ फैली तो लोगों ने सोशल मीडिया पर बजरंग दल से पूछा कि अगर हमला ही करना था तो आसाराम और राम रहीम जैसे बाबाओं के आश्रम पर क्यों नहीं किया जो कि बलात्कार ही कर रहे थे, और आश्रम में ही कर रहे थे। अब अगर ऐसे आश्रमों वाले देश में आश्रम पर एक वेब सीरीज बन रही है तो उस पर हमले से क्या सुधरेगा? खैर धर्म के कुकर्मों की बात कोई नई नहीं है, और आज इस मुद्दे पर यहां लिखने का एक मकसद यही है कि टेक्नोलॉजी दुनिया में एक ऐसा काम करने जा रही है जिससे कि हो सकता है धर्म के कुछ कुकर्म कम हो जाएं।
जर्मनी में अभी कुछ ईसाई चर्चों में एक रोबो पादरी का इस्तेमाल शुरु हुआ है जो कि अलग-अलग 5 भाषाओं में बाइबल के प्रवचन पढ़ सकता है, नसीहत में दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है, और धार्मिक संस्कार करवा सकता है। आज से 500 बरस पहले ईसाई धर्म में यूरोप भर में मार्टिन लूथर ने एक सुधारवादी आंदोलन शुरू किया था, और उसके 500 बरस पूरे होने के मौके पर यह रोबो प्रयोग के तौर पर कई चर्चों में इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर है कि चर्च जाने वाले लोगों की प्रतिक्रिया इस पर मिली-जुली हो सकती है, लेकिन चर्च के ढांचे के भीतर काम करने वाले पादरियों में इसे लेकर बेचैनी है। उन्हें लग रहा है कि उनके पेट पर लात पड़ने वाली है और उनका रोजगार छिनने वाला है। हालांकि हकीकत यह है कि पूरे यूरोप में पादरियों की कमी चल रही है, और चर्चों में धार्मिक संस्कार कराने को वे कम पड़ रहे हैं। ऐसे में यह पादरी रोबो 5 भाषाओं में संस्कार भी करवा सकता है, और जब हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है तो उससे प्रकाश की किरण भी निकलकर श्रद्धालुओं पर पड़ती है। हालांकि यह पूरी तरह मौलिक प्रयोग नहीं है क्योंकि कुछ बरस पहले चीन के एक बौद्ध मंदिर में एक रोबो भिक्षु का उपयोग शुरू किया गया था, जो कि मंत्र पढ़ता था, और धर्म की बुनियादी बातों को बोलता था।
अब यह रोबो जब तक किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ना हो जाए, और जब तक जिंदा पादरियों से यह कुछ बुरी बातें सीख न ले, तब तक तो यह भक्त जनों के लिए अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि आज दुनिया भर के चर्चों में पादरियों को बच्चों के यौन शोषण के आरोप झेलने पड़ रहे हैं. यूरोप के विकसित लोकतंत्रों में ऐसी घटनाएं लाखों में हुई हैं, यह बात खुद चर्च द्वारा करवाई गई जांच में सामने आई है न कि किसी चर्च विरोधी के लगाए गए आरोपों में। इसलिए फिलहाल तो ऐसे रोबो पादरियों से यह खतरा नहीं है कि वे बच्चों का यौन शोषण भी करेंगे लेकिन हो सकता है कि कभी इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया जाए, और उसके बाद ये असल पादरियों से सभी तरह की बातों को सीखें, और तब जाकर ये बच्चों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल इससे चर्च के भक्तों के बच्चों को एक सुरक्षित धार्मिक माहौल मिल सकता है।
अभी चर्च से जुड़े हुए पहलुओं में यह बहस चल रही है कि क्या धार्मिक संस्कारों का इस तरह मशीनीकरण करना ठीक है? अब हिंदुस्तान में अगर देखें तो यहां बहुत से हिंदू मंदिरों में बिजली की मशीनों से चलने वाले नगाड़े और ढोल मंजीरे इस्तेमाल होने लगे हैं, जो कि बिना भक्तों के भी अकेले पुजारी शुरू कर लेते हैं, और माहौल बन जाता है। हालांकि अभी पुजारी का विकल्प किसी रोबो में सामने नहीं आया है, लेकिन ढोल-मंजीरा बजाने वाले भक्तों का विकल्प तो मशीन में आ गया है। अब धीरे-धीरे यह भी हो सकता है कि जिस तरह किसी कॉमेडी शो में टीवी प्रसारण के पहले हंसने की आवाज, खिलखिलाने की, और तालियों की आवाज जोड़ दी जाती है, उसी तरह धर्म स्थलों में भी भक्तों की आवाजें जोड़ दी जाएं ताकि कम रहने पर भी वह बाहर से भक्तों की अधिक संख्या का झांसा दे सके। इसमें बुराई कुछ नहीं है क्योंकि धर्म कुल मिलाकर बहुत से लोगों को वैसे ही झांसा देता है, और अगर यह एक और झांसा देकर अधिक भीड़ का नजारा पेश करने लगे तो भी वह कोई पहला झांसा नहीं रहेगा।
अब वेटिकन गए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप को भारत आने का न्योता दिया है, और ऐसी कोई वजह नहीं है कि पोप भारत ना आएं क्योंकि यहां बड़ी संख्या में ईसाई आबादी है, और बड़ी संख्या में और लोगों को भी ईसाई बनाया जा सकता है, या कि वह बन सकते हैं, क्योंकि आज के उनके धर्म में उन्हें पावों का दर्जा देकर रखा गया है, और हो सकता है कि चर्च में उन्हें चर्च में थोड़ी बराबरी का मौका मिल जाए। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री की पार्टी पूरे देश में जगह जगह हिंदुओं के धर्मांतरण का जो आरोप लगाती है और जो जाहिर तौर पर चर्च पर लगाया जाता है, उसके मुखिया पोप का हिंदुस्तान आना कैसा माना जाएगा? खैर अगले कुछ बरस तो पोप को बुढ़ापे में भी दुनिया भर का दौरा करना पड़ेगा, और उसके बाद एक विकसित हो रही नई तकनीक मेटावर्स की मेहरबानी से लोग होलोग्राम की शक्ल में दुनिया में कहीं भी पहुंच सकेंगे, और वहां पर लोगों के बीच बैठकर किसी कार्यक्रम में शामिल भी हो सकेंगे। उस दिन हो सकता है कि पोप को हिंदुस्तान न आना पड़े, और उनके होलोग्राम से गले मिलकर मोदी उसका स्वागत कर सकें, या फिर यह भी हो सकता है कि मोदी का होलोग्राम जाकर पोप के होलोग्राम का गले लगकर स्वागत कर सके। और होलोग्राम आकर, जाकर स्वागत करेगा, तो उससे फादर से दूर रहने का मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक का फतवा भी निभा जाएगा क्योंकि मोदी को पोप से सीधे गले नहीं मिलना पड़ेगा। फिलहाल तो धर्म में टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर लोगों के बीच उत्सुकता से भरी जो बहस है जर्मनी से शुरू हुई है, उसे देखना चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
हिंदुस्तान में पिछले कुछ दिनों से सावरकर को लेकर एक बहस चल रही है। विनायक दामोदर सावरकर जिन्हें कुछ लोग वीर सावरकर भी कहते हैं और उन्हें वीर मानते हैं। दूसरी तरफ बहुत से दूसरे लोग हैं जिनका यह मानना है कि सावरकर अपनी जिंदगी के शुरू के हिस्से में तो स्वतंत्रता सेनानी रहे, लेकिन जैसे ही वे अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके अंडमान में काला पानी की सजा में भेजे गए उन्होंने तुरंत ही अंग्रेज सरकार से रहम की अपील करना शुरू कर दिया, और कुछ महीनों के भीतर उन्होंने ऐसी अर्जियां भेजना शुरू किया जो कि शायद कुल मिलकर पौन दर्जन तक पहुंचीं। इस बारे में अलग-अलग लेखों में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, इसलिए उन पूरी बातों को यहां दोहराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज की बात केवल सावरकर पर नहीं लिखी जा रही बल्कि इस बात पर लिखी जा रही है कि लोगों की जिंदगी को एक साथ, एक मुश्त देखकर उन पर एक अकेला लेबल लगाना कई बार मुमकिन नहीं होता है। गांधी के लिए जरूर ऐसा हो सकता था कि उनके पूरे जीवन को एक साथ देखकर भी उन्हें महात्मा लिखा जाए, लेकिन सावरकर को यह सहूलियत हासिल नहीं थी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम में शामिल रहे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जिस तरह उन्होंने लगातार माफी मांगी, लगातार रहम की अर्जी दायर की, और आखिर रहम मांगते हुए ही वे जेल से छूटे, और इतिहासकारों ने लिखा है कि उन्हें अंग्रेजों से हर महीने आर्थिक मदद भी मिली। अब ऐसे में जो लोग उनको वीर कहते हैं वह इतिहास के कुछ नाजुक पन्नों को कुरेद भी देते हैं जो उन्हें वीर साबित नहीं करते।
सावरकर का यह ताजा सिलसिला देश के सूचना आयुक्त उदय माहुरकर की सावरकर पर लिखी गई एक किताब के विमोचन के मौके पर शुरू हुआ जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां कि सावरकर ने रहम की अपील गांधीजी के कहे हुए लिखी थी। बहुत से इतिहासकारों ने उसके बाद लगातार यह लिखा कि जिस वक्त सावरकर ने रहम की अर्जियां भेजना शुरू कर दिया था, उस वक्त तो गांधी से सावरकर की मुलाकात भी नहीं हुई थी, गांधी हिंदुस्तान लौटे भी नहीं थे, वह दक्षिण अफ्रीका में ही थे, उस वक्त उनका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी कोई लेना देना नहीं था, और सावरकर को तो वे जानते भी नहीं थे। लेकिन इतिहास लेखन जब वक्त की सहूलियत के हिसाब से होता है तो उसमें कई तरह की सुविधाजनक बातों को लिख दिया जाता है और कानों को मधुर लगने वाले तथ्य गढ़ दिए जाते हैं। राजनाथ सिंह ने यह बात उदय माहुरकर की किताब को पढक़र नहीं कही थी क्योंकि उस किताब में इस बारे में कुछ जिक्र नहीं है, उन्होंने सावरकर पर अलग से यह बात कही।
यह सोचने समझने की जरूरत है कि जब लोगों की जिंदगी के अलग-अलग पहलू सकारात्मक और नकारात्मक, अलग-अलग किस्मों के होते हैं, उनमें कहीं खूबियां होती हैं और कहीं खामियां होती हैं, तो उनकी महानता को तय करना थोड़ा मुश्किल होता है। नायक और खलनायक के बीच में घूमती हुई ऐसी जिंदगी कोई एक लेबल लगाने की सहूलियत नहीं देती, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अब जैसे हिंदुस्तान के ताजा इतिहास को ही लें, तो कम से कम दो ऐसे बड़े पत्रकार हुए जो अखबारनवीसी में नामी-गिरामी थे, जिनके लिखे हुए की लोग तारीफ करते थे, और जिनके संपादन वाले अखबार या पत्रिका की भी तारीफ होती थी, लेकिन जब अपनी मातहत महिलाओं से बर्ताव की बात थी तो इसमें से एक संपादक ने अपनी एक मातहत कम उम्र लडक़ी के साथ जैसा सुलूक किया, उससे मामला अदालत तक पहुंचा, लंबा वक्त जेल में काटना पड़ा, और बाद में अदालत से उसे बरी किया गया। हिंदुस्तान में अदालत से बरी होने का मतलब बेकसूर हो जाना नहीं होता, बस यही साबित होता कि वहां पर पुलिस या जांच एजेंसी गुनाह साबित नहीं कर पाईं।
दूसरे संपादक के खिलाफ तो दर्जनभर या दर्जनों मातहत महिला पत्रकारों ने सेक्स शोषण की शिकायतें की हैं, और वह मामला अदालत में चल ही रहा है। अब किसी व्यक्ति की अच्छी अखबारनवीसी को उसके चरित्र के इस पहलू के साथ जोडक़र देखा जाए या जोडक़र न देखा जाए? यह सवाल बड़ा आसान नहीं है क्योंकि लोगों ने इतिहास में यह भी लिखा हुआ है कि हिटलर एक पेंटर था, और जिस तरह से उसने दसियों लाख लोगों का कत्ल किया, तो क्या उसकी बनाई किसी पेंटिंग को लेकर चित्रकला के पैमानों पर उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, या उसकी कोई बात नहीं करनी चाहिए? क्या गांधी महात्मा थे इसलिए उनके सत्य के प्रयोगों की चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या नेहरू देश के एक महान नेता थे इसलिए एडविना माउंटबेटन के साथ उनके संबंधों की चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या अटल बिहारी वाजपेई भाजपा के एक बहुत बड़े नेता थे, और जनसंघ से भाजपा तक अपने वक्त के वह सबसे बड़े नेता रहे, तो क्या उनकी जिंदगी में आई महिला के बारे में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए? या क्या इस बात को छुपाया जाना चाहिए कि वह शराब पीते थे? या नेहरू के बारे में यह छुपाना चाहिए कि वह सिगरेट पीते थे?
हिंदुस्तान एक पाखंडी देश है यहां पर लोग अपने आदर्श के बारे में किसी ईमानदार मूल्यांकन को बर्दाश्त नहीं करते। वे जिसे महान व्यक्ति या युगपुरुष मानते हैं, उसके बारे में किसी खामी की चर्चा सुनना नहीं चाहते। लेकिन हाल के वर्षों में हिंदुस्तान में एक नया मिजाज सामने आया है कि जिन लोगों को लोग नापसंद करें, उनके इतिहास और चरित्र के बारे में झूठी बातें गढक़र उन्हें तरह-तरह से, खूब खर्च करके, और खरीदे गए लोगों से चारों तरफ फैलाया जाए। किसी एक देश में किसी फैंसी ड्रेस में गांधी बना हुआ कोई आदमी किसी विदेशी महिला के साथ डांस कर रहा है तो उसे एक चरित्रहीन महात्मा गांधी की तरह पेश करने में हजारों लोग जुटे रहते हैं। अपनी बहन को गले लगाए हुए नेहरु की तस्वीर को चारों तरफ फैलाकर उन्हें बदचलन साबित करने की कोशिश में लोग लगे रहते हैं। ऐसे लोग अपने किसी पसंदीदा के बारे में एक लाइन की भी नकारात्मक सच्चाई सुनना नहीं चाहते, उस पर भी खून-खराबे को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नापसंद हैं उनके बारे में गढ़ी गई झूठी बातें भी फैलाने के लिए वे अपनी रातों की नींद हराम करते हैं।
झूठ के ऐसे सैलाब के बीच यह जरूरी रहता है कि इतिहास का सही इस्तेमाल हो, लोगों का सही मूल्यांकन हो, लोगों की खूबियों के साथ-साथ उनकी खामियों की चर्चा से भी परहेज न किया जाए, और किसी व्यक्ति को एक बिल्कुल ही बेदाग प्रतिमा की तरह पेश न किया जाए, क्योंकि गढ़ी गई प्रतिमा ही बेदाग हो सकती है, असल जिंदगी में तो इंसान पर कई किस्म के दाग लगे हो सकते हैं, जो कि कुदरत का एक हिस्सा हैं, कुदरत के दिए हुए बदन का एक हिस्सा, या कुदरत के दिए हुए मिजाज का एक हिस्सा।
सावरकर को लेकर जो लोग इतिहास के कड़वे हिस्से से परहेज कर रहे हैं, उनको लोकतंत्र की लचीली सीमाओं को समझना चाहिए जहां पर गांधी और नेहरू जैसे लोगों की कमियों और खामियों का भी जमकर विश्लेषण हुआ, और नेहरू के खिलाफ तो जितने कार्टून उस वक्त बनते थे, उनमें से कई मौकों पर वे कार्टूनिस्ट को फोन करके उसकी तारीफ भी करते थे। आज का वक्त ऐसा हो गया है कि नेहरू के मुकाबले बहुत ही कमजोर और खामियों से भरे हुए छोटे-छोटे से नेता उन पर बने हुए कार्टून पर लोगों को जेल डालने की तैयारी करते हैं। लोकतंत्र की परिपच्ता आने में हिंदुस्तान में हो सकता है कि आधी-एक सदी और लगे क्योंकि अब तो लोग यहां पर बर्दाश्त खोने लगे हैं, सच से परहेज करने लगे हैं, झूठ को गढऩे लगे हैं, और बदनीयत नफरत को फैलाने लगे हैं।
यह पूरा सिलसिला पूरी तरह अलोकतांत्रिक है और मानव सभ्यता के विकास की घड़ी के कांटों को वापिस ले जाने वाला भी है। सभ्य समाज और लोकतांत्रिक समाज को अपना बर्दाश्त बढ़ाना चाहिए, उसे लोगों के व्यक्तित्व और उनकी जिंदगी के पहलुओं को अलग-अलग करके देखना भी आना चाहिए और किसी का मूल्यांकन करते हुए इन सारे पहलुओं को साथ देखने की बर्दाश्त भी रहनी चाहिए। जो सभ्य समाज हैं वहां पर इतिहास लोगों को आसानी से शर्मिंदा नहीं करता। और जहां हिटलर जैसे इतिहास से शर्मिंदगी होना चाहिए तो वहां पूरा का पूरा देश, पूरी की पूरी जर्मन जाति शर्मिंदा होती है, और उससे मिले हुए सबक से वह सीखती है कि उसे क्या-क्या नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में लोगों के कामकाज से लेकर माफीनामे तक को लेकर जो लोग मुंह चुराते हैं, वो इतिहास की गलतियों को भविष्य में दोहराने की गारंटी भी कर लेते हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी एक ऐसी अफ्रीकी अमेरिकी महिला का सम्मान किया है जो 1951 में 31 बरस की उम्र में गुजर चुकी थी। उसे कैंसर था, और डॉक्टरों ने उसकी या उसके परिवार की इजाजत के बिना उसके कैंसर के कुछ सेल निकाल लिए थे। आज से करीब पौन सदी पहले लोगों के अधिकारों की इतनी खुलासे से बात नहीं होती थी, और डॉक्टरों ने उसके कैंसरग्रस्त सेल जब निकाल लिए, तो यह उस वक्त कोई मुद्दा नहीं बना। लेकिन अब जाकर हेनरिटा लैक्स नाम की इस महिला की स्मृति का सम्मान क्यों किया गया इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है।
इन कैंसरग्रस्त सेल को इस महिला के बदन के बाहर प्रयोगशाला में बढ़ाया गया और उन्हें कई गुना किया गया। बाद में दुनिया भर की अलग-अलग प्रयोगशालाओं ने, दवा कंपनियों ने इन सेल्स का इस्तेमाल पोलियो का टीका विकसित करने में किया, जींस का नक्शा बनाने में किया, और कृत्रिम गर्भाधान तकनीक में किया। इस महिला के कैंसरग्रस्त सेल का इतना व्यापक और महत्वपूर्ण इस्तेमाल हुआ कि आज इसे ‘आधुनिक चिकित्सा की मां’ नाम दिया गया।
इस महिला के कैंसरग्रस्त सेल का इस्तेमाल एचआईवी-एड्स की दवाइयां विकसित करने में भी किया गया और अभी कोरोना का इलाज ढूंढने में भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल इस महिला के सेल ऐसे पहले मानवीय सेल थे जिन्हें शरीर के बाहर क्लोन करके बढ़ाया गया। इसके पहले जितने कैंसर मरीजों के कैंसर सेल अस्पतालों में लिए जाते थे ताकि उन पर कोई शोध हो सके, तो वे तमाम नमूने 24 घंटे के भीतर दम तोड़ देते थे। लेकिन हेनरिटा लैक्स के सेल्स करिश्माई तरीके से जिंदा रहे और हर 24 घंटे में वे 2 गुना होते चले गए, इस तरह वे मानव शरीर के बाहर बढऩे वाले पहले कैंसर सेल थे, और इसलिए रिसर्च में उसका भारी इस्तेमाल हो सका। डब्ल्यूएचओ का हिसाब-किताब बताता है की हेनरिटा लैक्स के सेल अब तक 75000 से ज्यादा स्टडी में इस्तेमाल किए जा चुके हैं।
अभी इस महिला का सम्मान करते हुए स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि उसके बदन के सेल का खूब दोहन हुआ, और वह अश्वेत या काली महिलाओं में से एक थी जिनके शरीर का विज्ञान ने बहुत बेजा इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इस महिला ने अपने आपको चिकित्सा विज्ञान के हवाले किया था ताकि वह इलाज पा सके, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था ने उसके बदन के एक हिस्से को उसकी जानकारी और उसकी इजाजत के बिना लेकर उसका तरह-तरह से इस्तेमाल किया। चिकित्सा विज्ञान की खबरें बताती हैं कि इस महिला के नाम पर रखे गए इन कैंसर सेल, ‘हेलो’, का उपयोग उस सर्वाइकल कैंसर के इलाज में भी हुआ, जिस सर्वाइकल कैंसर की शिकार वह महिला थी।
अभी जब इस महिला के वंशजों का सम्मान हुआ, उसके 87 बरस के बेटे सहित कुनबे के कई लोग मौजूद थे, तो दुनिया के कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उसके परिवार को इसका मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि दवा कंपनियों ने उसके कैंसर सेल का इस्तेमाल करके टीके या दवाइयां बनाए, उनका खूब बाजारू इस्तेमाल हुआ। कुछ दूसरे लोगों का कहना था कि ऐसे बनाई गई सारी दवाइयों और सारे टीकों को बिना किसी मुनाफे के मानव जाति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।
अभी कुछ हफ्ते पहले इस परिवार ने ऐसी एक कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा किया है जिसने हेनरिटा लैक्स के कैंसर ग्रस्त सेल से दवा बनाकर अरबों रुपए कमाए हैं। परिवार का कहना है कि कंपनी इसे अपना बौद्धिक पूंजी अधिकार करार दे रही है। परिवार के वकील ने अदालत में यह मुद्दा उठाया कि किसी के शरीर का कोई हिस्सा कैसे उसकी इजाजत के बिना किसी दवा कंपनी की संपत्ति हो सकता है और इस महिला के सेल से विकसित की गई दवाइयों की कमाई का पूरा हिस्सा इस परिवार को दिया जाना चाहिए।
पश्चिमी दुनिया में चल रहे इस सिलसिले को देखें, तो लगता है कि हिंदुस्तान जैसे देश ऐसी भाषा से किस तरह पूरी तरह छूते हैं। यहां पर महिलाओं को जानवरों की तरह एक हॉल में लिटाकर उनकी नसबंदी कर दी जाती है, उनमें से कितनी जिंदा बचती हैं, और कितनी नहीं, इसकी कोई फिक्र नहीं होती। यहां इलाज के बीमे की रकम हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में गांव के गांव की जवान सारी महिलाओं को लाकर उनका गर्भाशय निकाल दिया जाता है, ताकि अस्पताल का बिल बन सके, और बीमा कंपनी से उसे वसूल किया जा सके। यहां कोई पूछने वाले भी नहीं रहते कि उस महिला को ऐसे ऑपरेशन की जरूरत थी या नहीं। किसी के बदन की कोई कीमत हो सकती है, उस पर उसका कोई हक हो सकता है, ऐसे तमाम मुद्दों से हिंदुस्तान मोटे तौर पर बेफिक्र रहता है। यहां बुनियादी इलाज के लिए आज भी सरकारी अस्पताल जाने वाले लोग उसे डॉक्टर और नर्सों का एक एहसान मानते हैं, फिर चाहे वह सरकारी अस्पताल ही क्यों ना हो। लोगों के नागरिक अधिकार इस कदर कुचले हुए हैं कि उनका हौसला ही नहीं होता कि वे कहीं अपने हक की बात गिना सकें। इसलिए हिंदुस्तान में किसी के शरीर के सेल अगर लिए भी जाते होंगे, तो शायद ही उसे इस बारे में कुछ बताया जाता होगा। और यह सिलसिला पश्चिम के पौन सदी पहले के इस सिलसिले जैसा आज भी यहां चल रहा होगा।
एप्पल कंपनी के नए मोबाइल फोन के बाजार में आने के पहले ही कंपनी की दी गई जानकारी कुछ घंटे के भीतर ही लोगों की जुबान पर आ जाती है कि अगला फोन किस साइज का आ रहा है, उसमें कौन सी खूबियां रहेंगी, और दाम कितने डॉलर रहेगा, यह हिंदुस्तान में वह कितने का पड़ेगा। शाहरुख खान का बेटा किसी नशे के मामले में पकड़ाता है तो उस बेटे के बारे में लोगों को खासी जानकारी रहती है। लेकिन हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े अखबार का खुद का बनाया हुआ एक पॉडकास्ट सुनते हुए अभी समझ आया कि उस अखबार के बड़े-बड़े दिग्गज राजनीतिक रिपोर्टर माइक्रोफोन पर बात करते हुए भी पंजाब के सिलसिले में दलितों को अलग गिन रहे हैं, और हिंदुओं को अलग। एक दलित के मुख्यमंत्री बनने के मामले को एक हिंदू मुख्यमंत्री से अलग गिनकर चल रहे हैं। यह मामला कुछ वैसा ही है कि कश्मीर के बारे में चर्चा करते हुए लोग कश्मीर और इंडिया जैसी बात करते हैं। एक अमरीकी रेडियो स्टेशन के लिए कुछ बरस पहले मैंने देश की एक बड़ी अखबारनवीस का ऑडियो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था जो कि कश्मीर के मामलों की बड़ी जानकार भी थीं, और उन्होंने बातचीत में एक से अधिक बार कश्मीर और इंडिया जैसी बातें कहीं, जाहिर है कि मेरा अगला और आखरी सवाल यही था कि क्या वे कश्मीर को इंडिया से अलग मानकर चल रही हैं ? और तब जाकर उन्हें अपनी चूक समझ में आई कि वे क्या गलती कर रही थीं।
अभी जब पंजाब में मुख्यमंत्री के बदलने की बात आई और एक दलित विधायक के मुख्यमंत्री बनने की मुनादी हुई तो बहुत से खासे पढ़े लिखे लोगों को हैरानी के साथ यह चर्चा करते हुए सुना कि क्या सिखों में भी कोई जाति व्यवस्था है? लोग यही मानकर चल रहे थे कि जिस तरह गुरुद्वारे की पंगत में बिना जाति धर्म पूछे सबको एक साथ खाना खिलाया जाता है तो उससे शायद सिखों के भीतर कोई जाति व्यवस्था नहीं होगी। सच तो यह है कि भारत के किसी भी दूसरे प्रदेश के मुकाबले पंजाब में दलितों की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है, वहां 32 फीसदी दलित हैं। लेकिन लोगों की याददाश्त कुछ कमजोर रहती है और मीडिया के बहुत से लोगों ने टीवी चैनलों पर यह कहा, और अखबार की खबरों में भी लिखा, कि यह पंजाब का पहला गैर-सिक्ख मुख्यमंत्री बनने जा रहा है जबकि इसके पहले पंजाब में एक से अधिक गैर-सिक्ख मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लोगों की जानकारी असल मुद्दों को लेकर धीरे-धीरे कम इसलिए हो रही है कि फिल्म इंडस्ट्री के एक अभिनेता की खुदकुशी को राजनीतिक बनाने की कोशिशों में वे डूब जाते हैं। खेल सत्तारूढ़ ताकतें करती हैं और लोग स्टेडियम में बैठे दर्शकों की तरह मैच देखने जाते हैं, लेकिन चीयरलीडर्स की तरह नाचने लगते हैं। अफवाहों और झूठ-फरेब के इस बाजार में सच की इज्जत इतनी कम रह गई है कि लोग खबरों में सच पाने की उम्मीद करते, न कोशिश करते।
अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है जिसमें किसी महानगर में कॉलेज के छात्र-छात्राओं के बीच एक कैमरा और माइक्रोफोन लिए हुए लोग उनसे हिंदुस्तान के बारे में कई किस्म के सवाल करते हैं। उन्हें हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम, पहले राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम, उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री का नाम नहीं मालूम, उन्हें छत्तीसगढ़ के भीतर झारखंड है या झारखंड के भीतर छत्तीसगढ़ है यह भी नहीं मालूम, उन्हें उत्तराखंड, हिमाचल, और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग होने की खबर नहीं है, उन्हें किसी बात की खबर नहीं है, और वे खासे फैशनेबल कपड़े पहने हुए, संपन्न परिवारों के, कॉलेज में पढ़ रहे या पढ़ चुके लोग दिख रहे हैं। जो सामान्य ज्ञान के दसियों सवालों में नाकामयाब हो कर कैमरे से ही यह सवाल करते हैं कि क्या यह उन्हें अपमानित करने के लिए यह किया जा रहा है?
हिंदुस्तान के असल मुद्दों की जानकारी में लोगों की दिलचस्पी बहुत ही कम है। सच तो यह है कि लोगों की अपने आसपास की ऐसी जानकारी में दिलचस्पी नहीं है जिससे उन्हें कोई मजा नहीं मिलता। देश के बड़े-बड़े अखबारों के छत्तीसगढ़ में रहने वाले रिपोर्टरों से कई बार यह कहा जाता है कि वे बहुत दुख-तकलीफ की या नक्सल हिंसा की खबरें बहुत अधिक ना भेजें क्योंकि उनमें किसी की अधिक दिलचस्पी नहीं है। जब मरने वाले गिनती में बहुत अधिक होते हैं, तब तो यह खबर बनती है, लेकिन छोटी-मोटी नक्सल हिंसा की खबरों में किसी अखबार की दिलचस्पी नहीं रहती, छत्तीसगढ़ के अखबारों की भी सीमित दिलचस्पी रहती है। इसके पीछे की वजह यह है कि विज्ञापन देने वाले लोग अखबार या टीवी चैनलों को दुख-दर्द, तकलीफ, और लाशों से भरा हुआ देखना नहीं चाहते। उसकी जगह एक किसी जहाज पर चल रही पार्टी में थोड़ा-बहुत नशा कर रहे लोगों के पकडाने पर शाहरुख खान के बेटे की वीडियो के साथ कई-कई घंटे उसी खबर को दिखाने में टीवी चैनलों की दिलचस्पी अधिक है, और हो सकता है कि अखबार भी वैसे ही निकलें।
फिल्मी दुनिया, सेक्स, क्राइम, और क्रिकेट से जुड़ी हुई खबरें लोगों को गुदगुदाती हैं, और उन्हें कुछ भी सोचने पर मजबूर नहीं करती। यह कुछ वैसा ही होता है कि सोफे पर बैठ कर चिप्स खाते हुए टीवी पर क्रिकेट देखना जितना आरामदेह रहता है, कसरत करना या दौडऩा, साइकिल चलाना तो उतना आरामदेह हो नहीं सकता। इसलिए लोग अपने दिमाग पर अधिक जोर डालना नहीं चाहते, अपने भीतर के सामाजिक सरोकारों को जगाने का खतरा भी उठाना नहीं चाहते। सामाजिक सरोकार अगर जाग गए तो देश-दुनिया के असल मुद्दे उनके दिल-दिमाग को परेशान करने लगेंगे। इसलिए ऐसी खबरों को ही ना पढ़ा जाए कि कितने लोग कुपोषण के शिकार हैं, कितने बच्चे पिछली शाम के खाने के बाद अगला खाना अगली दोपहर स्कूल में ही पाते हैं। ऐसी खबरों को पढऩे के बाद लोगों के अपने गले से कुछ उतरना मुश्किल होने लगेगा इसलिए लोग सामाजिक सरोकार की तमाम बातों से दूर रहते हैं।
यही वजह है कि दलितों के मुद्दों की जानकारी लोगों को कम है. कश्मीर में एक सैलानी जितनी दिलचस्पी तो है, लेकिन कश्मीर के लोगों की बाकी दिक्कतों से लोग अपने को दूर और अछूता रखते हैं. लोग उत्तर-पूर्वी राज्यों की दिक्कतों से अपने को दूर रखते हैं, और दिल्ली के बाजारों में उत्तर-पूर्व के लोगों को देखकर उन्हें चिंकी बुलाकर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। लोगों को उन लोगों को देख कर भी आत्मग्लानि होती है जो कि बहुत सादगी से जीते हैं, इसलिए ममता बनर्जी की साधारण रबड़ चप्पल और उसकी साधारण साड़ी को लोग मखौल का सामान मानते हैं, और जो नेता दिन में 4 बार, 6 बार महंगे कपड़े बदलते हैं, उनकी वे इज्जत करते हैं। लोग नेताओं से यह पूछना नहीं चाहते कि उनके पास इतना पैसा कहां से आया, और लोग देश के गरीबों की तकलीफ को जानना नहीं चाहते कि बिना पैसों के या इतने कम पैसों के साथ वे जिंदगी कैसे काट सकते हैं।
लोगों का सामाजिक सरोकार से दूर रहना, लोगों की तकलीफों को अनदेखा करना, जमीन की कड़वी हकीकत को नहीं देखना, इन सबसे लोग सुखी रहते हैं, और यही वजह है ये मुद्दे धीरे-धीरे खोते जा रहे हैं फीके पड़ते जा रहे हैं। इसे एक और बात से जोडक़र देखा जा सकता है कि किस तरह हिंदुस्तान की संसद में अरबपति बढ़ते चले जा रहे हैं, और हिंदुस्तान की विधानसभाओं में भी करोड़पतियों का अनुपात लगातार बढ़ते चल रहा है। इतनी संपन्नता लोगों को विपन्नता के दर्शन ही नहीं करने देती और बहुत गरीबी से तकरीबन अनजान लोग जब संसद या विधानसभा में बैठकर चर्चा करते हैं, तो जाहिर है कि वह चर्चा गरीबों पर तो टिक नहीं सकती, वहां तक पहुंच भी नहीं सकती। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
हिमाचल के शिमला की एक खबर है कि वहां एक आदमी अपनी बीवी को व्हाट्सएप पर चैटिंग से रोकता था, और इस बात को लेकर उसकी बीवी खासी खफा थी, झगड़ा बढ़ा तो पत्नी ने डंडा लेकर पति की जमकर पिटाई की और उसके तीन दांत भी तोड़ दिए। पति ने जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और पत्नी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। यह मामला पिटाई और दांत तोडऩे तक पहुंचने की वजह से खबरों में आ गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर जीवनसाथी की सक्रियता को लेकर शादीशुदा जिंदगी के तनाव का यह अकेला मामला नहीं है। आज मोबाइल फोन और कंप्यूटर की मेहरबानी से सोशल मीडिया पर लोग कई किस्म से दुनिया भर के दूसरे लोगों से जुड़ रहे हैं, और उसका नतीजा कई किस्म के जुर्म में भी तब्दील हो रहा है, और कई किस्म के पारिवारिक या सामाजिक तनाव में भी।
हिंदुस्तान में हर दिन किसी न किसी प्रदेश से खबर आती है कि वहां किसी हिंदुस्तानी ने विदेशी बनकर, या किसी एक धर्म के व्यक्ति ने दूसरे धर्म का प्रोफाइल बनाकर किस तरह किसी शादीशुदा महिला को, या किसी महिला ने किसी बुजुर्ग आदमी को फंसाया, शादी का, सेक्स का, प्यार का, या साथ रहने का झांसा दिया, और बात आगे बढ़ते-बढ़ते इतनी बढ़ी कि लोग घर के गहने चोरी करके देने लगे, अपनी जमीन-जायदाद बेचकर मांग पूरी करने लगे, और बहुत से मामलों में अपने नाजुक पलों की तस्वीरें या वीडियो एक दूसरे को भेजने लगे, जिन्हें लेकर आगे ब्लैकमलिंग का सिलसिला शुरू हो गया।
दुनिया के बहुत से दूसरे देशों के मुकाबले हिंदुस्तान में यह नौबत कुछ अधिक इसलिए आ रही है कि यहां का समाज सदियों से औरत और मर्द को दूर रखते आया है, लडक़े लड़कियों को मिलने से रोकते आया है, और अब जब सोशल मीडिया ने या कंप्यूटर और मोबाइल फोन की मैसेंजर सर्विस ने दुनिया भर के लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया है, तो लोग अपने पारिवारिक संबंधों से परे भी एक खुशी ढूंढने लगे हैं, और बहुत से मामलों में पाने भी लगे हैं। यह मान लेना गलत होगा कि सोशल मीडिया और मैसेंजर से बने हुए ऐसे नए रास्तों ने लोगों का महज नुकसान किया है। आज बहुत से लोग ऐसे बाहरी रिश्तों की वजह से एक आत्मसंतुष्टि में जीने लगे हैं, उन्हें यह बाहरी चाह खुश रखने लगी है, निराशा से दूर कामयाबी की तरफ बढ़ा भी रही है। अब फर्क केवल यह पड़ रहा है कि शादीशुदा जिंदगी में भागीदारों की एक दूसरे से जो उम्मीदें रहती हैं, और वफादारी की जो परंपरागत सोच है, उसे परे जाकर ऐसे ऑनलाइन संबंध विकसित हो जाते हैं जो कि शादीशुदा जिंदगी की घुटन से तो लोगों को उबार लेते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ दूसरे नए खतरे भी खड़े कर देते हैं।
दुनिया के अधिक विकसित देशों में औरत-मर्द का पहले से बाहर साथ-साथ काम करना चले आ रहा था, वहां पर यह समस्या उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन भारत जैसा समाज जिसमें महिलाओं का एक बड़ा तबका घर पर ही रह जाता है, और देश के कुल कामकाजी लोगों में महिलाएं सिर्फ 15 फीसदी हैं. ऐसे में हिंदुस्तान में अधिकतर महिलाएं घर पर रहती हैं जिन्हें अभी कुछ बरस पहले तक बाहर किसी से संपर्क का जरिया कम ही रहता था, लेकिन अब मोबाइल फोन, दुपहिया गाडिय़ों, थोड़ी बहुत बाहर आवाजाही के चलते हुए लोगों को दूसरों से मिलने का मौका भी मिलता है, और सोशल मीडिया की वजह से लोगों की दोस्ती भी होती है। चूँकि हिंदुस्तान में संचार तकनीक के ये सामान और सोशल मीडिया इन दोनों का इतिहास बहुत लंबा नहीं है, और कम से कम विकसित देशों के मुकाबले तो बहुत ही नया है, इसलिए यहां पर लोग अभी सोशल मीडिया को जरूरत से अधिक महत्व भी देते हैं, और वहां पर मिले हुए नए लोगों से बड़ी तेजी से करीब भी आ जाते हैं।
शिमला की है ताजा घटना एक नए किस्म का सामाजिक माहौल भी बताती है। अगर पति की शिकायत पूरी तरह सच है, और जैसा कि पुलिस ने तुरंत जुर्म कायम किया है, तो उसकी पत्नी एक नए किस्म का अधिकार भी इस्तेमाल कर रही है। हिंदुस्तान में महिलाएं आमतौर पर पिटते आई हैं, और इस मामले में इस महिला ने पति को पीटकर उसके दांत तोड़ दिए हैं। तो यह समानता का माहौल एक नई बात है, और सोशल मीडिया या मैसेंजर पर चैटिंग, फोटो या वीडियो का लेना-देना एक नए सामाजिक तनाव की बात है।
मनोवैज्ञानिक हिसाब से देखें तो यह पूरा सिलसिला इसलिए परिवार के आपसी संबंधों के मुकाबले अधिक महत्व पा जाता है कि परिवार के ढांचे में आने के बाद लोगों के आपसी संबंध परिवार की दिक्कतों से लद जाते हैं, और जब तक लोग महज सोशल मीडिया या मैसेंजर पर एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, वे अपना सबसे अच्छा रुख सामने रखते हैं जो कि कई बार झूठा भी रहता है, कई बार बनावटी या दिखावटी रहता है। लेकिन फिर भी इंसान का मन है जो उसे सुहाने वाली चीजों को सुनहला सच भी मान लेता है। इसलिए लोग सोशल मीडिया पर बने हुए संबंधों में एक दूसरे को मुखौटों के पीछे से मिलते हैं, और वहां दोनों अपनी अपनी पारिवारिक दिक्कतों से लदे हुए नहीं रहते हैं। यही वजह रहती है कि सोशल मीडिया के रिश्ते बहुत से लोगों को असल जिंदगी के लदे हुए, बोझ बने हुए रिश्तों के मुकाबले अधिक आकर्षक लगते हैं, और अपने-आपको दिया जा रहा है यह धोखा, दूसरे लोगों से धोखा खाने का खतरा भी दे जाता है।
इस मुद्दे पर हमारे पास तुरंत ही कोई राय नहीं है क्योंकि जीवन शैली धीरे-धीरे बदलती है, और धीरे-धीरे बदली जा सकती है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी की आंधी आकर जिंदगी की भावनाओं को तहस-नहस कर देती है, तब लोग उस आंधी की रफ्तार से संभल नहीं पाते हैं। लोग शुरुआती वर्षों में एक ऑनलाइन खुशी के दौर में डूब जाते हैं, और अपने परिवार के लोगों के मुकाबले उन्हें बाहर के लोगों का मुखौटा कभी-कभी बेहतर भी लगने लगता है। ऐसे में उन परिवारों में असर अधिक होता है जो पहले से तनाव झेल रहे हैं, जहां जिंदगी पहले से बोझ बनी हुई है। वहां सोशल मीडिया या मैसेंजर पर मिलने वाली राहत एक मरहम की तरह काम करती है, और लोगों को जिंदा रहने का या जीने का एक नया मकसद मिल जाता है।
बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं जिनको सोशल मीडिया पर मिलने वाले महत्व की वजह से उन्हें एक नया आत्मगौरव हासिल होता है जो कि घर में चली आ रही जिंदगी में मिलना बंद हो चुका रहता है। घर के लोगों के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर रहती है, और सोशल मीडिया के मुखौटे के पीछे से एक-दूसरे से मिलने वाले लोगों को दाल भी मुर्गी जैसी लगती है, क्योंकि वहां लोग अपना सबसे अच्छा सजाया हुआ चेहरा सामने रखते हैं, और किसी तरह का बोझ है एक दूसरे के लिए नहीं रहता है। असल जिंदगी में तो होता है यह है कि जीवन साथी एक साथ, एक कमरे में रहते हुए, एक-दूसरे के बदन से निकलने वाली तमाम किस्म की आवाज, और तमाम किस्म की गंध को झेलने के लिए मजबूर रहते हैं। दूसरी तरफ ऑनलाइन बने हुए संबंधों में लोग एक-दूसरे को अपना मेहनत से गढ़ा हुआ एक ऐसा चेहरा दिखाते हैं जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहता है, न वहां डकार की आवाज आती है, और न पसीने की बदबू।
इस मुद्दे पर लिखना अंतहीन हो सकता है, लेकिन आज लिखने का मकसद यह है कि लोगों को ऑनलाइन या सोशल मीडिया के संबंध को एक हिफाजत की दूरी के साथ ही बनाना चाहिए, ताकि वे तबाही का सामान ना बन जाए। लोगों को ऑनलाइन होने वाले धोखे की खबरों को पढऩा चाहिए, और किस तरह लोग ऑनलाइन रिश्तों के बाद ब्लैकमेलिंग के शिकार होते हैं, दूसरे किस्म के जुर्म के शिकार होते हैं इस बारे में भी पढऩा चाहिए। जुर्म की कहानियां हमेशा ही जुर्म के लिए उकसाने वाली नहीं होती हैं, कई बार वे लोगों को सावधानी सिखाने वाली भी होती हैं। इसलिए लोगों को ऐसे मामलों की चर्चा अपने आसपास के दायरे में जरूर करनी चाहिए, ताकि उनके करीबी लोगों में से कोई अगर ऐसे किसी जुर्म का शिकार होने के करीब पहुंचे हुए हों, तो कम से कम वे तो बच जाएं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने कर्नाटक के एक जज को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम में देश की न्याय व्यवस्था को लेकर फिक्र जाहिर की और कहा कि यह अंग्रेजों के दौर से चली आ रही व्यवस्था है, जिसके भारतीयकरण की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की समस्याओं पर अदालतों की वर्तमान कार्यशैली कहीं से भी फिट नहीं बैठती है। उन्होंने कहा कि गुलामी के समय की न्याय व्यवस्था चली आ रही है और अदालतों में अंग्रेजी में कानूनी कार्रवाई चलती है जिसे ग्रामीण या और लोग नहीं समझ पाते, इसलिए भी किसी केस पर उनके अधिक पैसे खर्च होते हैं। उनका कहना है कि न्यायपालिका का काम ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी को कोर्ट और जज से किसी भी तरह का डर नहीं लगे।
जस्टिस एनवी रमना लगातार कई किस्म की सकारात्मक बातें कर रहे हैं, और अदालत में भी उनका रुख सरकार के हिमायती किसी जज का न होकर जनता के हित का दिखता है, और ऐसा साफ नजर आता है कि वह सरकार का चेहरा देखकर ठकुरसुहाती के अंदाज में बातें नहीं करते हैं। वे सरकार से कड़े सवाल करके जवाब-तलब करने में नहीं हिचकते हैं। इसलिए उनकी बातों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए क्योंकि पिछले कई वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कम ही हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश जनता के हितों के पक्षधर दिखे हैं, और सरकार को खुश करने की कोई नीयत उनकी नहीं दिखी है। लेकिन जिस जज को श्रद्धांजलि देने के लिए वे पहुंचे थे उस जज की कई खूबियों को भी उन्होंने गिनाया और हम उस बारे में भी आज इस कॉलम में लिखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस मोहन एम शांतनगौदर एक ऐसे असाधारण जज थे, जो बहुत काबिल भी थे लेकिन वे दयालु थे और उदार थे। जस्टिस रमना ने बताया कि किस तरह उन दोनों ने किसी बेंच पर एक साथ रहते हुए कई महत्वपूर्ण मामलों में फैसले लिए थे, जिनमें मौत की सजा पाए हुए दोषियों के मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा भी शामिल रहा।
जस्टिस रमना की कही हुई इन बातों से परे भी भारत की न्यायपालिका में बहुत सारी चीजें हैं जिनमें सुधार की जरूरत है, और हो सकता है कि देश के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए वे इस मामले में दखल दे सकें, और चीजों को बेहतर बना सकें। चूँकि उन्होंने अंग्रेजों के समय की छोड़ी गई गुलामी के दिनों की परंपराओं को लेकर यह चर्चा की है, इसलिए यह याद रखना जरूरी है कि हिंदुस्तान के अधिकतर हिस्सों में साल के अधिकतर महीनों में गर्मी रहती है, और अदालतों के कमरे, खासकर छोटी अदालतों के, जिला अदालतों के कमरे, वकीलों के चैम्बर, अदालतों गलियारे, एयर कंडीशंड नहीं रहते हैं। ऐसे में वकीलों और जजों को काले कोट कर पहनकर काम करने के लिए कहना एक बड़ी ज्यादती रहती है। बहुत से गरीब वकील जिनके पास सिर्फ एक कोट रहता है वे अपने काले कोट पर पसीने के दाग लिए हुए काम करते हैं, क्योंकि वे रोज उसे धुलवा भी नहीं सकते।
इससे परे एक दूसरी चीज यह है कि निचली अदालतों में तो हमारे देखने की यह आम बात है कि जजों के ठीक सामने बैठे हुए उनके बाबू किसी तारीख को बढ़ाने के लिए या कोई भी रियायत ना चाहने वाले गवाह या वादी, प्रतिवादी किसी के भी आने पर वहां उसकी हाजिरी भी लगाने के लिए नगद रिश्वत लेते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन जजों की नजर में यह न आता हो। ऐसे में यह मानने की कोई वजह नहीं है कि ऐसी रिश्वत में उन जजों का हिस्सा नहीं रहता। देश के मुख्य न्यायाधीश गरीब और ग्रामीण लोगों को अदालतों में होने वाली तकलीफ की बात करते हैं तो यह तो एक बहुत बड़ी तकलीफ है जो कि अधिकतर प्रदेशों की निचली अदालतों में खुलकर सामने दिखती है। ऐसा नगद रिश्वत का लेन-देन भी अगर कोई जज अपनी आंखों के सामने नहीं रोक पाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को, और मुख्य न्यायाधीश को इस बारे में सोचना चाहिए।
अदालतों से दहशत की एक बड़ी वजह यह भी है कि कई वकील वादी, प्रतिवादी को बुरी तरह निचोड़ लेते हैं और अदालतों के बाबू तो उनकी हालत खराब कर ही देते हैं। निचली या ऊपर की हर किस्म की अदालतों में जजों के भ्रष्ट होने की आशंका बहुत से लोग समय-समय पर जाहिर करते आए हैं और लोगों को याद होगा कि किस तरह देश के कानून मंत्री रहे हुए शांति भूषण और उनके वकील बेटे प्रशांत भूषण ने एक वक्त सुप्रीम कोर्ट के आधा दर्जन से अधिक जजों के भ्रष्ट होने का आरोप लगाया था। अदालत ने उन पर अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाया था, उन पर कई तरह से दबाव डाला गया था कि वे माफी मांगें, ताकि इस मामले को खत्म किया जा सके, और बाप-बेटे ने किसी भी माफी मांगने से इंकार कर दिया था। लेकिन उनकी बात का नैतिक दबाव इतना था कि शायद अदालत ने आज तक उस मामले का निपटारा ही नहीं किया है, और ऐसा सच आरोप लगाने वाले शांति भूषण और प्रशांत भूषण को सजा देने की हिम्मत शायद अदालत की नहीं पड़ी, और वह मामला अभी तक खड़ा हुआ है। अगर अदालतों में वकीलों से चर्चा की जाए, और अलग-अलग किस्म के अलग-अलग दर्जे के बहुत से वकीलों से चर्चा की जाए, तो यह साफ पता लग जाता है कि कितने जज रिश्वत नहीं लेते हैं। कुछ मौके ऐसे भी आए हैं जब किसी एक हाईकोर्ट के कई वकीलों से चर्चा करने पर यह भी सुनने मिला कि वहां एक भी जज के ईमानदार होने की उन्हें कोई खबर नहीं है। अब अगर देश के मुख्य न्यायाधीश अदालतों को जनता के प्रति दोस्ताना बनाना चाहते हैं, अदालतों की दहशत खत्म करना चाहते हैं, तो भ्रष्टाचार तो एक बहुत ही ठोस मुद्दा है जो कि एक जुर्म भी है, और सजा के लायक जुर्म है। इसलिए उन्हें सबसे पहले न्यायपालिका से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक अभियान चलाना चाहिए। हमारा ऐसा मानना है कि इसके लिए एक मौलिक सूझबूझ की जरूरत भी पड़ेगी क्योंकि यह इतना संगठित काम हो चुका है, इसकी जड़ें इतनी गहरी बैठ चुकी हैं, कि कोई एक मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यकाल में इसे पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी बात का समाधान उस दिन शुरू होता है जिस दिन उस समस्या के अस्तित्व को मान लिया जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में और अधिक खुलकर बोलें, और अधिक खुलकर चर्चा करें। न्यायपालिका और वकीलों के बीच में इस बात को लेकर एक विचार विमर्श शुरू हो कि भ्रष्टाचार को कैसे खत्म, या कम किया जा सकता है। उनकी इस बात से हम सहमत हैं कि अदालत के नाम से ही आम लोगों के मन में दहशत आ जाती है। जो मुजरिम हैं वहीं अदालत में सबसे अधिक आत्मविश्वास से और सबसे अधिक बेफिक्री से घूमते हैं।
भारत की न्यायपालिका को लेकर एक बात जिसे सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बिना किसी नीतिगत फैसले के एक मामूली आदेश से ही सुधार सकते हैं। आज भारत की बड़ी अदालतों में जजों के लिए योर ऑनर, या मी लॉर्ड जैसे सामंती शब्दों का इस्तेमाल चल रहा है जो कि अंग्रेजों के समय से शुरू हुआ है। या सिलसिला पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है और एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच में दर्जे का इतना बड़ा फासला खड़ा कर देता है कि नीचे खड़े हुए लोग दहशत में आ ही जाते हैं। इसलिए अदालत की भाषा से ये अलोकतांत्रिक शब्द पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। देश के मुख्य न्यायाधीश को यह भी देखना चाहिए कि अभी कुछ बरस पहले प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति बनने पर राष्ट्रपति के लिए संबोधन में महामहिम शब्द का इस्तेमाल खत्म करवा दिया था, जो कि पूरी तरह से अंग्रेजी राज के सामंतवाद का एक प्रतीक था। इसके बाद देश के बहुत से राज भवनों में भी राज्यपाल के लिए महामहिम शब्द का इस्तेमाल बंद हुआ, और अगर कहीं चल रहा होगा तो उसकी जानकारी अभी हमको नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जजों के काले लबादे, जजों के लिए अलग किस्म के राजसी पोशाक वाले चपरासी, इन सब का सिलसिला खत्म करना चाहिए। जजों को अधिक से अधिक इंसान की तरह रहना चाहिए ताकि बाकी इंसान उनसे दहशत ना खाएं।
इस सिलसिले में हमको एक शानदार मिसाल याद पड़ती है जो कि हिंदुस्तान के जजों को थोड़ा सा आहत भी कर सकती है। लेकिन जब कभी हम सुधार की बात करेंगे तो कुछ ना कुछ लोग तो आहत होंगे ही। अमेरिका के एक राज्य रोड आइलैंड में प्रोविडेंस नाम की जगह पर एक म्युनिसिपल कोर्ट के एक जज हैं जिनका नाम फ्रैंक कैप्रियो है। दिलचस्प बात यह है यह स्थानीय अदालत मोटे तौर पर ट्रैफिक के चालान का निपटारा करती है, और यहां तक वही लोग आते हैं जो लोग ट्रैफिक पुलिस, या स्थानीय पार्किंग अधिकारियों के किए गए चालान का जुर्माना जमा नहीं करते हैं, और इस अदालत तक पहुंचते हैं। अब इस छोटी सी अदालत के बारे में हमको जानकारी ऐसे मिली कि इस अदालत की कार्यवाही का जीवंत प्रसारण अमेरिका में होता है और भारत के लोगों के लिए यह बात अकल्पनीय हो सकती है कि एक स्थानीय म्युनिसिपल कोर्ट के ट्रैफिक मामलों के निपटारे को देखने के लिए अमेरिका में करोड़ों लोग अलग-अलग टीवी चैनलों पर इसका प्रसारण देखते हैं। अमेरिका के सैकड़ों टीवी चैनल अपने-अपने इलाके में इस अदालत की कार्यवाही का जीवंत प्रसारण करते हैं और वहां के किसी भी दूसरे लोकप्रिय टीवी प्रोग्राम के मुकाबले फ्रैंक कैप्रियो के निपटारे को देखने वाले दर्शक कम नहीं हैं।
अब इस जज की कार्रवाई देखें तो वे सबसे पहले वहां पहुंचने वाले, चालान पाए हुए लोगों की बेचैनी, घबराहट, और उनके डर को खत्म करते हैं। उनसे दोस्ताना लहजे में बात करते हैं, उनका नाम पूछते हैं, उनका काम पूछते हैं, उनके साथ आए हुए बच्चों या बड़ों से उनका रिश्ता समझते हैं, और अक्सर ही साथ आए हुए बच्चों को ऊपर जज के स्टेज पर बुलाकर उनसे दोस्ती करते हैं, उनको पूरा मामला समझाकर उनसे राय लेते कि उनके परिवार के व्यक्ति से कितना जुर्माना लिया जाए या जुर्माना न लेकर क्या उसे छोड़ दिया जाए? वे उन हालात को समझते हैं जिनमें किसी से ट्रैफिक नियमों के खिलाफ गाड़ी चलाना हो गया है, या गलत जगह पर गाड़ी पार्क करना हो गया है। उनकी वजह को समझकर, उनके काम को समझकर समाज में उनके योगदान को समझकर, या उन पर परिवार के असाधारण बोझ को जानकर वे कई मामलों में जुर्माने से माफी दे देते हैं, और लोगों को हंसी-खुशी वापस रवाना कर देते हैं। कई मामलों में जहां उनको जुर्माना जरूरी लगता है लेकिन यह समझ आता है कि चालान पाने वाले लोग जुर्माना पटाने की हालत में ही नहीं है, वे बेरोजगार हैं, या उन पर बच्चों का और बीमारों का बहुत बोझ है, तो वे दुनिया भर से उनके पास पहुंचने वाले मदद के दान का इस्तेमाल करते हैं, और दानदाता का नाम पढ़ कर उनके भेजे गए चेक से वह जुर्माना जमा करवाते हुए, गरीब या बेबस लोगों को जुर्माने से बरी कर देते हैं, और भेज देते हैं।
जज फ्रैंक कैप्रियो के अदालती वीडियो 2017 में डेढ़ करोड़ लोगों ने देखे थे 2020 में वह बढक़र तीन करोड़ हो गए और यूट्यूब पर उनके वीडियो 4।30 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं, और आगे बढ़ा चुके हैं। उनकी हंसमुख शक्ल में जज की कुर्सी पर बैठा हुआ एक ऐसा इंसान लोगों को दिखता है, जो किसी के किए हुए मामूली ट्रैफिक गलत काम को देखने के साथ-साथ उनकी स्थितियों को समझता है, परिस्थितियों को समझता है, उनकी बेबसी-मजबूरी को समझते हुए उसका बहुत ही मानवीय आधार पर निपटारा करता है। मैंने खुद ने पिछले कुछ महीनों में उनके सैकड़ों ऐसे प्रसारण देखे हैं जो कि फेसबुक पर भी मौजूद हैं, और यूट्यूब पर भी। इनको देख कर लगता है कि एक अदालत में भी कितनी इंसानियत हो सकती है, और अदालत में कटघरे में खड़े किए गए लोगों को भी किस तरह से इंसान समझा जा सकता है, और उनके दुख-दर्द में हाथ बंटाया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के दूसरे जजों को इस प्रसारण को देखने की सलाह उन्हें अपना अपमान भी लग सकता है, लेकिन हर जज दिन में कुछ मिनट तो कम से कम टीवी पर कुछ ना कुछ देखते होंगे, तो इसे एक फिल्मी कहानी मानकर ही देख लें, इसे हमारी नसीहत मानकर ना देखें, इसे अपने ऊपर कोई नैतिक दबाव मानकर न देखें, और इसे देखने के बाद अगर उन्हें ठीक लगे तो वे सोचें कि जिस बात को आज भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है, क्या उस बात के साथ अमेरिका की छोटी सी म्युनिसिपल अदालत का कोई तालमेल उन्हें दिखता है?
पिछले कई महीनों से मैं इस कॉलम में इस अदालत के बारे में लिखना चाह रहा था, और इसे भारत की न्यायपालिका के लिए एक मिसाल बनाकर भी सामने रखना चाह रहा था। वह लिखना हो नहीं पाया था लेकिन अभी जिस तरह से भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी भावना सामने रखी है, और हमारा ऐसा मानना है कि देश के मुख्य न्यायाधीश की भावना अदालत के फैसलों को काफी दूर तक प्रभावित भी कर सकती है, इसलिए देखें कि क्या अमेरिका की एक म्युनिसिपल कोर्ट का एक जज जो कि अमेरिका से बाहर भी करोड़ों लोगों का दिल जीत चुका है, क्या वह भारत की न्यायपालिका को भी सोचने का कुछ सामान दे सकता है?
पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ अखबारनवीसों के बीच यह बहस छिड़ी है कि जिन लोगों को सही वाक्य लिखना नहीं आता, उन्हें मीडिया में लिखने का हक है, या नहीं। बहस के शब्द कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन कुल जमा बात भाषा को लेकर है कि उसका सही होना कितना जरूरी है। और यह बहस कोई नई नहीं है, हमेशा से बातचीत में कुछ लोग जब किसी की काबिलीयत को चुनौती देते हैं, तो यही कहते हैं कि उसे एक वाक्य भी ठीक से लिखना नहीं आता। जो लोग अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पाते हैं, उनके बारे में अंग्रेजी के जानकार कहते हैं कि वे दो वाक्य भी बिना रूके नहीं बोल पाते, और सही तो बोल ही नहीं पाते।
अब अंग्रेजी में इन दिनों एक शब्द का चलन कई जगह दिखाई पड़ता है, ग्रामर-नाजी। ग्रामर तो व्याकरण है, और नाजी है नस्ल के आधार पर नफरत करने वाला, हिटलर का अनुयायी। तो जो लोग ग्रामर की गलतियों को एक नस्लभेदी नफरत के साथ हिकारत से देखते हैं, उन लोगों के लिए ग्रामर-नाजी शब्द गढ़ा गया है। और यह बात हिन्दुस्तान में हिन्दी भाषा में भी है, जो कि देश के बहुत से हिन्दीभाषी राज्यों की स्थानीय बोलियों से मिलकर बनी भाषा है, और जिस पर क्षेत्रीयता या स्थानीयता का प्रभाव भी खासा कायम है। हिन्दी का व्याकरण तो गढ़ लिया गया है, लेकिन क्षेत्रीय बोलियों के शब्द अलग-अलग इलाकों में चलते हैं, जिनके कि कोई विकल्प नहीं हैं, और बहुत से ऐसे क्षेत्रीय बोली के शब्द हैं, जिनके कोई बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकते।
इसके साथ-साथ भाषा की एक बड़ी खूबी कहावत और मुहावरा भी होते हैं। ऐसी लोकोक्तियों के बिना कोई भी भाषा अधूरी रहती है, और अधिकतर लोकोक्तियां किसी न किसी क्षेत्रीय भाषा से निकली हुई रहती हैं, और उनकी शब्दावली से लेकर उनके व्याकरण तक में आज की खड़ी बोली कही जाने वाली हिन्दी के पैमाने पर कई गलतियां निकाली जा सकती हैं।
भारत जितने बड़े देश को देखें, और यहां के अलग-अलग हिन्दीभाषी प्रदेशों की मूल और मौलिक बोलियों को देखें, तो आज की आम हिन्दी उन सबका एक उसी तरह का संघीय ढांचा है, जिस तरह का ढांचा अमरीकी राज्यों का मिलकर यूनाईटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका बनता है, या जिस तरह भारत एक संघीय गणराज्य है, या जिस तरह एक वक्त सोवियत संघ था। आज हिन्दी उसी तरह की एक भाषा है, जिसके भीतर बोलियों के अपने-अपने साम्राज्य अब तक कायम हैं।
आज बिहार के लालू यादव की हिन्दी देखें, और उधर हरियाणा के किसी जाट की हिन्दी देखें, और इधर मुलायम सिंह की हिन्दी देखें, तो ऐसा लगेगा कि हम कई अलग किस्म की जुबानों की बात कर रहे हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि बहुत से अलग-अलग देशों को मिलाकर यूरोपीय यूनियन बना है।
अब ऐसे में एक सही वाक्य जिसे न आए, वह अखबारनवीसी न करे, या अखबारनवीसी के लायक नहीं है, यह एक ऐसा शहरी, उच्च-शिक्षित, कुलीन और आभिजात्य पैमाना है जो कि आम लोगों को लिखने के हक से बाहर कर देता है। ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ग्रामर-नाजी लोगों का हक छीन पा रहे हैं, या कि क्षेत्रीय अखबारों में वहां की बोलियों के प्रभाव वाली हिन्दी पूरी तरह से नकार दी गई है। ऐसा होना उन लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती भी होगी जिन्होंने हिन्दी के संघीय ढांचे के साथ-साथ अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व को भी कायम रखा है, और अपनी क्षेत्रीय बोली की खूबी के साथ वे हिन्दी का इस्तेमाल करते हैं। यह याद रखने की जरूरत है कि खड़ी बोली वाली हिन्दी क्षेत्रीय बोलियों की जिन बातों को हिन्दी में खामी करार देती है, वे तमाम खामियां उन क्षेत्रीय पैमानों पर खूबियां भी हो सकती हैं।
लेकिन यह पूरी बातचीत भाषा पर हो गई। आज की इस बात का मकसद अखबारनवीसी की जुबान पर है। एक अच्छी भाषा और एक सही व्याकरण वाली भाषा में फर्क भी हो सकता है। ये दोनों कहीं-कहीं पर एक भी हो सकती हैं, और कहीं-कहीं अलग भी। बहुत से लोगों की हिन्दी एकदम सही हो सकती है, कुछ लोगों की हिन्दी मेरी तरह कुछ खामियों वाली भी हो सकती है, और कुछ लोगों की हिन्दी खासी खामी वाली होते हुए भी बड़ी असरदार हो सकती है। और ये खामियां अगर क्षेत्रीय-खूबियां हैं, तो उनके सामने सही व्याकरण कोई मुद्दा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
अखबार की जुबान में व्याकरण का एक महत्व जरूर होना चाहिए, लेकिन वह महत्व जुबान की बाकी बातों से ऊपर होना भी जरूरी नहीं है। जुबान का असरदार होना, न्यायसंगत होना, और अखबारी बातों को पाठक तक सही तरीके से पहुंचाने में कामयाब होना व्याकरण से कम महत्वपूर्ण नहीं है, शायद अधिक ही महत्वपूर्ण है।
जिन लोगों को एक वाक्य सही लिखना नहीं आता, उन लोगों को अखबारनवीसी नहीं करना चाहिए, ऐसा पैमाना क्षेत्रीय बोली से सीखकर अखबारनवीसी में आए अधिकतर लोगों को बेरोजगार कर देगा। और यह बहुत बड़ी बेइंसाफी भी होगी। जिन लोगों को हिन्दी के लिए ऐसा दुराग्रह है, या किसी भी भाषा के व्याकरण के लिए जिनकी ऐसी जिद है, उनको यह समझना चाहिए कि दुनिया की बहुत सी भाषाओं में व्याकरण, हिज्जों, और उच्चारण के अनगिनत अपवाद ऐसे रहते हैं जिन्हें स्थानीय इस्तेमाल के आधार पर तय किया जाता है। अंग्रेजी को ही लें, जिसमें इतने अधिक अपवाद हैं कि उसे सीखने वाले लोगों की नानी ही मर जाती है। और ऐसे तमाम अपवादों को न्यायसंगत ठहराने के लिए अंग्रेजी जुबान के जानकार यह तर्क देते हैं- बिकॉज नेटिव्स से सो, (चूंकि स्थानीय लोग ऐसा कहते हैं)।
भारत की हिन्दी को आज की आधुनिक हिन्दी के व्याकरण की कैद में बांधकर, उसके कम जानकार लोगों को हिकारत से देखना एक बड़ी बेइंसाफी है। अगर किसी की हिन्दी ऐसे शहरी-आधुनिक पैमाने पर खरी है, तो वे उस पर गर्व कर सकते हैं। लेकिन जिनकी हिन्दी क्षेत्रीय पैमानों पर खरी है, उनको भी अपनी भाषा पर गर्व करने का उतना ही हक है। हिन्दी को एक संघीय ढांचे की तरह क्षेत्रीय बोलियों का सम्मान करते हुए एक संपर्क-भाषा की तरह काम करना चाहिए, तो ही हिन्दी राष्ट्रभाषा है। अगर वह क्षेत्रीय खूबियों को नीची नजर से देखते हुए व्याकरण का अपना एक फौलादी ढांचा क्षेत्रीय बोलियों पर लादने का आग्रह करेगी, तो वह अपने ही वजन को घटा बैठेगी।
और जहां तक हिन्दुस्तान के हिन्दी इलाके की अखबारनवीसी की जुबान की बात है, तो उसका तो हिन्दी होना भी जरूरी नहीं है। उसकी लिपि देवनागरी हो सकती है, लेकिन उसकी जुबान एक मिली-जुली हिन्दुस्तानी हो सकती है जैसी कि खड़ी बोली के आने के पहले मुगलों के साथ आई उर्दू के चलन के बाद, और फिर अंग्रेजों की जुबान का तडक़ा लगने पर मिलकर चल रही थी। क्षेत्रीय बोलियों का अलग-अलग तरह का मेल अलग-अलग इलाकों में था, और उनमें से कोई भी क्षेत्रीय बोली आज की खड़ी बोली हिन्दी से कमजोर नहीं थी। उन बोलियों में असर हिन्दी से कहीं अधिक था, और भारत की गैरहिन्दी क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में भी हिन्दी के मुकाबले अधिक वजनदार, अधिक पैने, और अधिक असरदार शब्द हैं, और जुमले हैं।
आज सोशल मीडिया पर अंग्रेजी या हिन्दी, या कोई और जुबान, इन सबके इस्तेमाल में भाषा और ग्रामर के तमाम नियम-कायदों को जिस तरह उठाकर फेंक दिया गया है, और ऐसा सोशल मीडिया बड़े-बड़े भाषा-पंडितों के लिखे हुए के मुकाबले अधिक असर का हो गया है, उससे भाषा की शुद्धता के धर्मान्ध लोगों को इस शुद्धता के सीमित महत्व को समझ लेना चाहिए। आज सबसे अधिक इस्तेमाल हो रहे, और सबसे अधिक असरदार सोशल मीडिया पर न ग्रामर रह गया, न हिज्जे रह गए, न उच्चारण रह गए, और न ही परंपरागत शब्द या वाक्य-विन्यास रह गए। कुछ बरसों के भीतर ही लोगों के बीच के संवाद ने एक निहायत ही अलग औजार विकसित कर लिया जिसे कि शुद्धतावादी भाषा भी कहने से इंकार कर देंगे। लेकिन यह समझना चाहिए कि भाषा को गढ़ा ही इसलिए गया था कि लोग एक-दूसरे तक अपनी बात पहुंचा सकें, दूसरों की बात समझ सकें। यह एक बड़ा ही सीमित इस्तेमाल था, और इस सीमित इस्तेमाल के लिए शुद्धतावादियों ने भाषा को आग में तपा-तपाकर चौबीस कैरेट सोने की तरह खरा करने की कोशिश की, कर भी लिया, लेकिन उसके बिना भी लोग बखूबी अपना काम चला ले रहे हैं।
एक वक्त था जब लोकसंगीत और लोकनृत्य को तपा-तपाकर, आग में पकाकर, उसे नियमों में बांधकर, उसकी लय और ताल को शास्त्रीयता के पैमाने तक ले जाया गया, और कला को एक दरबारी दर्जा दिया गया, उसे समझ पाने वाले लोगों को पारखी का दर्जा दिया गया, और उसे आम लोगों के सीखने-समझने के दायरे से बाहर निकाल दिया गया। कुछ ऐसा ही भाषा के व्याकरण की शुद्धता को लेकर किया गया। लेकिन जिस तरह लोककला और लोकसंगीत अब दीवारों को कैनवास बनाने लगे हैं, रेलवे स्टेशनों पर म्यूजिक-बैंड बनने लगे हैं, वे आज भी किसी शास्त्रीयता के मोहताज नहीं हैं।
इसलिए सही व्याकरण वाला वाक्य एक अच्छी बात हो सकती है, एक अनिवार्य बात नहीं हो सकती। और अखबारनवीसी में तो अकेला दुराग्रह सिर्फ सच और इंसाफ के लिए होना चाहिए, जुबान तो निहायत गैरजरूरी है। दो दिन पहले सीरिया से जान बचाकर भागे परिवार का एक बच्चा जिस तरह समंदर के किनारे लाश की शक्ल में कैमरे में कैद हुआ है, और जिसे देखकर पूरी दुनिया हिल गई है, उस तस्वीर में फोटोग्रॉफी के व्याकरण की खूबियों और खामियों की तरफ किसी का ध्यान जाता है? और जिस वक्त यह तस्वीर ली गई होगी, उसी वक्त दुनिया के बहुत से फोटोग्राफर मेहनत करके, फोटोग्रॉफी के पैमानों का ध्यान रखते हुए तस्वीरें ले रहे होंगे, लेकिन उनकी हजार गुना अधिक जानकारी, मेहनत, इस बेमेहनत तस्वीर के मुकाबले इतिहास में कहीं दर्ज नहीं हो पाएगी।
मायने यह रखता है कि किसी लिखे हुए, कहे हुए शब्द, या दिखाई हुई फिल्म या तस्वीर में सच कितना है, और उसमें इंसाफ की गुजारिश कितनी है। वरना शुद्धता दुनिया के किसी काम की नहीं है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
अमेरिका में अभी एक नई बहस छिड़ी है कि जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हें हवाई जहाज में चढऩे दिया जाए या नहीं? वहां सरकार ने वैक्सीन लगवाने का फैसला तो लोगों पर छोड़ा है, लेकिन वहां भारत जैसी हालत भी नहीं है कि विमान में चढऩे के पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना पड़े या कोरोना नेगेटिव होने का सर्टिफिकेट दिखाना पड़े। अमेरिका में लोग अपनी निजी स्वतंत्रता को लेकर अधिक जागरूक या, बेहतर होगा यह कहें कि, अधिक अडिय़ल है। उनमें से बहुत से लोग तो मास्क लगाने से भी इंकार कर देते हैं कि यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। वैक्सीन न लगवाने वाले भी बहुत से जिद्दी लोग हैं जिनका कई किस्म का तर्क रहता है। लेकिन महज अमेरिकी लोगों को ही जिद्दी क्यों कहें, हिंदुस्तान के इतिहास को देखें तो जब कस्तूरबा गांधी की तबीयत बहुत खराब हुई थी, और पुणे के आगा खान महल में वे महात्मा गांधी के साथ रखी गई थीं, तब अंग्रेज डॉक्टर उन्हें देखने आया था। उसने जब पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाने की तैयारी की तो गांधी उससे इस बहस में उलझ गए कि किसी दवा को इंजेक्शन से शरीर में डालना प्रकृति के खिलाफ है। और इनके बीच कुछ बातचीत के बाद वह इंजेक्शन नहीं लग पाया, और दवा मौजूद रहते हुए भी कस्तूरबा चल बसी थीं। तो गांधी की जिद ने कस्तूरबा की जान ले ली थी। आज भी गाँधी होते तो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाते क्योंकि वह प्रकृति के खिलाफ होती। उसी तरह अमेरिका में बहुत से लोग जिद पर अड़े हुए हैं कि वे वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। लेकिन दूसरे लोगों का कहना है कि वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों का नुकसान और खतरा वे लोग क्यों झेलें जो कि वैक्सीन लगवा चुके हैं? बात सही भी है, गैरजिम्मेदार लोगों के हिस्से का नुकसान जिम्मेदार लोग क्यों झेलें ?
लेकिन अमेरिका और टीकों से परे की बात देखें तो भी दुनिया भर में यह देखने मिलता है कि किसी कार्यक्रम में समय पर पहुंचने वाले लोग अपने वक्त की बर्बादी करते उन लोगों का इंतजार करने को मजबूर रहते हैं जो देर से आने की आदत रखते हैं और कार्यक्रम जिनके लिए इंतजार करते रहता है। और तो और अपनी खुद की शादी में दूल्हा-दुल्हन कई बार दावत में इतनी देर से पहुंचते हैं कि वहां आए हुए मेहमान उनके इंतजार में खड़े रहते हैं। किसी बैठक में भी यही होता है कि समय पर पहुंचे हुए लोग अपने मन में खुद को और लेट-लतीफ लोगों को कोसते हुए बैठे रहते हैं, और देर से आने वाले लोग मजे से हंसते-मुस्कुराते पहुंचते हैं।
जो लोग सिगरेट-बीड़ी नहीं पीते हैं, उन्हें किसी जगह पर मौजूद दूसरे ऐसे लोग तकलीफ देते हैं, लेकिन ऐसे अनचाहे धुंए को झेलने के लिए मजबूर लोग नुकसान पाते हुए वहां खड़े या बैठे रहते हैं। हिंदुस्तान में यह सिलसिला इतना अधिक है कि बहुत से लोगों को यह अफसोस होता है कि वे इतने असभ्य देश में पैदा क्यों हुए हैं जहां एक काल्पनिक इतिहास के ऊपर तो सबको गर्व है, लेकिन आज मौजूद शर्मनाक वर्तमान पर किसी को शर्मिंदगी नहीं है। अभी छत्तीसगढ़ में भाजपा की एक बड़ी नेता और छत्तीसगढ़ की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि भाजपा के लोग एक बार थूक दें तो भूपेश बघेल की पूरी सरकार बह जाएगी। बात सही भी हो सकता है क्योंकि भाजपा छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी होने का दावा करती है, और उसके बहुत से लोग तंबाकू-गुटखा खाकर इतना इतना थूक उगलते हैं कि हो सकता है कि एक सैलाब आ जाए। जो लोग सार्वजनिक जगहों पर नहीं थूकते हैं उन्हें ही दूसरों का ऐसा थूका हुआ अधिक खटकता है। जो लोग हर कुछ देर में किसी ना किसी साफ-सुथरी और सार्वजनिक जगह को देखकर थूकने में लग जाते हैं, उन्हें तो भला क्या बुरा लगता होगा।
किसी संपन्न कॉलोनी में भी रहने वाले लोगों को आसपास के असभ्य पड़ोसियों और उनके मेहमानों की बदतमीजी को झेलना पड़ता है, जिनकी गाडिय़ां आड़ी-तिरछी खड़ी रहती हैं, जो घरों के बाहर जोर-जोर से फिजूल की बात करते हुए मोबाइल फोन लिए टहलते रहते हैं, आते जाते घर की घंटी की जगह हॉर्न बजाते हैं और रास्ता रोकते हैं, और अड़ोस-पड़ोस की दीवार पर पेशाब करने में जुट जाते हैं। ऐसे लोग गिनती में बहुत कम रहते हैं जो अपने घर आने वालों या अपने मेहमानों को तमीज याद दिलाने की जहमत उठाएं। अधिकतर लोग दूसरों के प्रति किसी भी जिम्मेदारी को लेकर पूरी तरह बेफिक्र रहते हैं और अपने अधिकारों का दावा करने के लिए उतने ही चौकन्ने रहते हैं।
हिंदुस्तानी लोगों का यह मिजाज बड़ा ही दिलचस्प है कि हर सुबह अपने घर-दुकान के सामने का कचरा झाड़ू से सडक़ के दूसरी तरफ कर दें, मानो सडक़ एक सरहद है और उसकी दूसरी तरफ कोई दुश्मन देश है। एक बार दुनिया के सभ्य देशों में जाकर जो हिंदुस्तानी लौटते हैं उनका मोटा-मोटा अंदाज यह रहता है कि वहां जैसी सभ्यता, वहां जैसी साफ-सफाई और साफ हवा, तमीज हिंदुस्तान में सैकड़ों बरस तक नसीब नहीं होनी है। यहां पर लोग दूसरे लोगों की गंदगी और गलतियों की तकलीफ भुगतने के लिए मजबूर रहते हैं, और गंदगी फैलाने वाले, परेशानी फैलाने वाले लोग इस हद तक बेशर्म रहते हैं कि उन्हें शायद इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वह कुछ गलत कर रहे हैं।
हिंदुस्तान की सडक़ों पर देखें तो दारु पिए हुए या दूसरे किस्म के नशे में गाड़ी चलाने वाले लोगों की संख्या कम नहीं रहती है। लेकिन लोग उन्हें रोक नहीं सकते क्योंकि रोकने का काम पुलिस का है, और पुलिस उन्हें कई वजहों से नहीं रोकती क्योंकि एक तो उसकी क्षमता इतनी गाडिय़ों और ड्राइवरों को जांचने की नहीं है, दूसरा यह कि इनमें से जो पिए हुए रहते हैं उनसे कुछ कमाई हो जाती है, इसलिए भी वह उन्हें जाने देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सडक़ों पर पिए हुए लोग दूसरों पर खतरा रहते हैं। वे अपनी जान खतरे में डालें न डालें, दूसरों को कुचल सकते हैं। ऐसे में सडक़ों पर जिम्मेदारी से चलने वाले लोगों के क्या अधिकार हैं जिससे वे पिए हुए या नशे में लोगों को रोक सकें ? जो जिम्मेदार हैं उनके कोई अधिकार नहीं है, और जो गैरजिम्मेदार हैं उन पर कोई रोक नहीं है। हिंदुस्तान में सार्वजनिक जगहों का यही हाल है।
लोग अपने बच्चों को महंगी गाडिय़ां खरीद कर देते हैं जिनमें से बच्चे किसी के साइलेंसर फाड़ देते हैं, किसी के हेडलाइट को बदल देते हैं, किसी में प्रेशर हॉर्न लगवा लेते हैं, और दूसरों का जीना हराम करते चलते हैं। कभी-कभार भूले-भटके कोई अफसर ऐसी कुछ दर्जन गाडिय़ों पर कोई कार्यवाही करवा दे तो करवा दे, वरना आमतौर पर किसी को इनमें कोई बुराई नहीं दिखती क्योंकि हमारा मिजाज ही ऐसा हो गया है कि इस देश में तकलीफ पाना लोगों की बदनसीबी है, पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है, और इसमें सरकार का या किसी और का दखल देना ठीक नहीं है।
कुल मिलकर जिम्मेदार लोगों की किस्मत में भड़ास में जीने के अलावा और कुछ नहीं है। अगले जन्म में किसी सभ्य देश में पैदा होने के लिए इस जन्म में कुछ नेक काम करते चलें।(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
सुप्रीम कोर्ट ने अभी महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक पत्रकार की याचिका पर जिला प्रशासन का यह आदेश खारिज कर दिया जिसमें इस पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता को जिला बदर किया गया था। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में अमरावती में पुलिस और प्रशासन से मिलकर पत्रकार रहमत खान को अमरावती शहर या अमरावती ग्रामीण जिले में एक साल तक न आने-जाने का आदेश दिया था। जिला बदर के इस आदेश के खिलाफ यह पत्रकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और अदालत ने सरकार के इस आदेश को खारिज करते हुए कहां कि किसी व्यक्ति को देश में कहीं भी रहने या स्वतंत्र रूप से घूमने के उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
लोगों को याद होगा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं या राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, मजदूर नेताओं को, जिला बदर करने को जिला प्रशासन और पुलिस एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। देश के तकरीबन सभी राज्यों में प्रशासन जिला बदर के अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानून को डराने के लिए भी इस्तेमाल करता है और अपने को नापसंद लोगों को जिले से निकाल देने की एक ऐसी सजा देता है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना हर किसी के बस का नहीं रहता। छत्तीसगढ़ में कई दशक पहले पीयूसीएल नाम के मानवाधिकार संगठन के एक बड़े कार्यकर्ता राजेंद्र सायल ने इस बात को कई जगह उठाया था कि जिला बदर करने का कानून संविधान में बताए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने कई मंचों पर इस बात को उठाया था, और इस बारे में लिखा भी था। लेकिन पुलिस और प्रशासन को प्रतिबंध के सारे तौर-तरीके बहुत सुहाते हैं क्योंकि उन्हें आसानी से लादा जा सकता है, और सत्तारूढ़ नेताओं को उनके फायदे को गिनाया जा सकता है। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ नेता पुलिस और प्रशासन की मदद से अपनी राजनीति चलाते हैं और इसलिए वे तमाम किस्म के प्रतिबंधों की प्रशासन की पहल के हिमायती भी रहते हैं।
इस प्रतिबंध को ही देखें तो अगर कोई व्यक्ति किसी जिले में वहां के लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन जाता है तो उसे उस जिले से बाहर रहने के लिए पर्याप्त कारण मानते हुए उसे जिला बदर कर दिया जाता है। अब कुछ देर के लिए, बहस के लिए यह मान भी लें कि कोई व्यक्ति एक जिले में इतना बड़ा गुंडा हो जाता है, अपराधी हो जाता है कि वहां के लोगों को उससे खतरा रहता है, और उसे जिले से बाहर निकाल देना जिले की हिफाजत के लिए जरूरी लगता है। ऐसे में सवाल यह है कि जो एक जिले के लिए खतरा है उसे उस जिले से निकालकर उसे दूसरे जिले पर खतरा बनाकर क्यों डालना चाहिए? और फिर जिले की सुरक्षा तो अधिकारियों का जिम्मा है, कोई एक व्यक्ति इतना खतरनाक हो सकता है कि वह उस जिले से निकाल देने के लायक हो जाए? दिलचस्प बात यह है कि अभी जिस व्यक्ति को अमरावती से जिला बदर किया गया था उसने सरकार में कई तरह की सूचना के अधिकार की अर्जियां लगाई थीं और कई शैक्षणिक संस्थाओं और मदरसों में हुई आर्थिक अनियमितता के बारे में जानकारी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट में रहमत खान नाम के इस कार्यकर्ता ने तर्क दिया कि उसके खिलाफ यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उसने सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को खत्म करने और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए कदम उठाया था। उसका कहना है कि कलेक्टर और पुलिस से उसने ऐसे दुरुपयोग की जांच का अनुरोध किया था और इसके बाद इन संस्थाओं से जुड़े लोगों ने उसके खिलाफ एक रिपोर्ट लिखाई थी।
अमरावती जिला प्रशासन और पुलिस का यह रुख बताता है कि अफसर अपने अधिकारों का कैसा बेजा इस्तेमाल करते हैं, और हो सकता है कि राजनीतिक ताकतें भी ऐसे भ्रष्टाचार को बचाने के पीछे रहती हों। पुलिस और सत्तारूढ़ नेताओं के बीच का गठबंधन पूरे देश के हर राज्य में इतना खतरनाक हो चुका है कि अभी दो-चार दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ एक टिप्पणी भी की है। छत्तीसगढ़ के एक आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ऐसी बहुत सी बातें कहीं। अदालत ने देश के कई राज्यों के ऐसे मामलों के बारे में कहा कि जब कोई सरकार जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो पिछली सरकार के करीबी अफसरों के खिलाफ कई तरह के मामले दर्ज होने लगते हैं, यह हिंदुस्तान में एक नया रुख देखने में आ रहा है। देश के बहुत से राज्यों में ऐसा हो रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी को नापसंद लोगों के खिलाफ तरह-तरह के फर्जी मामले दर्ज कर लिए जाते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देनी पड़ी जिसमें राज्य सरकार द्वारा दंगाइयों के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिए गए, और उसके लिए हाईकोर्ट से लेने इजाजत लेने की शर्त भी पूरी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हाईकोर्ट की इजाजत के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है।
पुलिस और प्रशासन के हथियार अंग्रेजों के वक्त बनाए गए ऐसे बहुत से कानून हैं जिन्हें कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बताया जाता है, लेकिन जो मोटे तौर पर एक विदेशी जुल्मी सरकार के अत्याचार जारी रखने के लिए अंग्रेजों के वक्त पर बनाए गए थे। आज भी हिंदुस्तान की अफसरशाही, यहां की पुलिस उन्हें जारी रखने के पक्ष में हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे बहुत से कानूनों को खत्म करने की बात करती है, कई कानूनों को खत्म किया भी गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी की पार्टी ही कई प्रदेशों की अपनी सरकारों में लोगों के खिलाफ बड़ी रफ्तार से राजद्रोह के मामले दर्ज करती है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बरसों पहले फैसला दे चुका है। अभी सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली का ही एक मामला चल रहा है जिसमें जब अदालत ने यह पूछा कि कुछ छात्रों के खिलाफ राजद्रोह का मामला कैसे दर्ज किया गया, तो पुलिस ने कुछ टीवी चैनलों का नाम लिया कि वहां वीडियो देखकर पुलिस ने उन पर राजद्रोह का मामला लगाया। जब इन चैनलों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्विटर पर कुछ ट्वीट में यह वीडियो देखकर उन्हें अपने समाचारों में दिखाया था। और जब उन ट्वीट की जांच की गई तो यह पता लगा कि उन्हें भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख ने ट्वीट किया था, और वहां से लेकर वे समाचार चैनलों में दिखाए गए, और वहां से उन वीडियो को देखकर पुलिस ने राजद्रोह के मुकदमे दर्ज कर लिए थे।
अब यह वक्त आ गया है कि पूरे देश में पुलिस और प्रशासन के ऐसे मनमानी करने के अधिकार खत्म किए जाएं, ऐसे कानून खत्म किए जाएं जिनमें कानून-व्यवस्था बनाए रखने जैसे बहुत ही अमूर्त और अस्पष्ट किस्म के बहाने गिनाकर लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाती है, और लंबे समय तक उन्हें परेशान किया जाता है। आज क्या इस बात की कल्पना की जा सकती है कि किसी मामूली व्यक्ति को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया जाए तो किस तरह वह अपने जिले के बाहर रहेगा, कैसे जिंदा रहेगा, उसे कौन काम देगा, और किस तरह उसका परिवार उसके बिना साल भर जिंदा रह सकेगा? ऐसी नौबत की सोचे बिना सिर्फ सरकारी बहाने बनाकर ऐसी कार्रवाई पूरी तरह पूरी तरह से नाजायज है और इस पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया है जो जिला बदर करने की कार्रवाई के खिलाफ एक व्यापक टिप्पणी की है जो कि जिला बदर के बाकी मामलों में भी देशभर मैं इस्तेमाल की जा सकेगी। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
पुराने कानूनों और नई टेक्नोलॉजी ने दुनिया के साथ-साथ भारत के लिए कई किस्म की नई चुनौतियों खड़ी कर दी हैं। अमरीका जैसे कुछ देश जिन्होंने टेक्नोलॉजी बदलने की रफ्तार से ही कानून भी बदल लिए, वे भी आज इन नए कानूनों के कई पहलुओं से रोज जूझ रहे हैं। इंटरनेट ने लोगों की जिंदगी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहुत से ऐसे नए पहलू जोड़े हैं जिनके बारे में कुछ बरस पहले तक मीडिया का एकाधिकार सा बने रहने की वजह से कभी सोचने की नौबत नहीं आई थी। अब बहुत मामूली से खर्च के साथ कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर जाकर वहां अपने मन की बहुत किस्म की बातें लिख सकते हैं, दूसरे लोगों को महान या घटिया बता सकते हैं। इस नई आजादी ने कल तक अखबारों के संपादक नाम की एक सेंसरशिप को खत्म कर दिया है और अब लोग सीधे-सीधे दूसरे लोगों तक पहुंच जाते हैं, पल भर में, सभी सरहदों को चीरकर।
भारत सरकार बीच-बीच में नोटिस देकर इंटरनेट की बहुत सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों को देकर कहती है कि वे वहां से आपत्तिजनक सामग्री हटाएं। दूसरी तरफ देश की कई बड़ी अदालतें भी ऐसे ही नोटिस इन वेबसाइटों को देती रहतीं हैं, जो मोटे तौर पर पश्चिमी दुनिया से चलती हैं, और समय-समय पर दुनिया के अलग-अलग देशों के प्रतिबंध झेलने की आदी हैं। फेसबुक, ट्विटर और इसी किस्म की दूसरी बहुत सी वेबसाइटें लोगों के बीच बातचीत, विचार-विमर्श और गाली-गलौज का रिश्ता मुहैया कराती हैं। पिछले एक-दो दशकों में भारत की सरकार को अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने किस्म के आंदोलन झेलने पड़े उनमें जनमत को तैयार करने और बात को फैलाने में इन वेबसाइटों ने खासी मदद की। नतीजा यह है कि सरकार इन पर लोगों की लिखी बातों से नाखुश है। लेकिन बात महज इतनी नहीं है। बिना किसी रोक-टोक के जब लोगों को अपनी किसी भी तरह की दिल-दिमाग की हालत के चलते लिखने और नेट पर डाल देने की सहूलियत है, और जब तक कोई कानूनी जांच न हो तब तक लोगों को एक यह छूट भी मिली हुई है कि वे बेनामी, गुमनामी के साथ, किसी नकली नाम से भी यह काम कर सकते हैं, तो नतीजा यह कि लोग किसी की वल्दियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो किसी की मां के चाल-चलन की बात कर रहे हैं।
हमारा अपना अनुभव यह रहा है कि यह बेकाबू आजादी जितना भला कर रही है उतना ही एक ऐसा बुरा भी कर रही है जिसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई इस टेक्नोलॉजी के बेसरहद होने से मुमकिन भी नहीं है। भारत की सरकार अगर किसी वेबसाइट को रोक भी देगी, तो दुनिया के बहुत से देशों ने ऐसा करके देख लिया है, उससे कुछ नहीं थमता। तो ऐसे में इस मर्ज का इलाज क्या है? अभी मोदी सरकार ने एक नया आईटी कानून बनाकर उन्हीं सोशल मीडिया के पर कतरने की कोशिश की है, जिन पर सवार होकर वह दो-दो बाद सत्ता पर पहुंची है।
दरअसल इंटरनेट लोगों को बिना अपनी शिनाख्त उजागर किए लिखने की एक ऐसी छूट देता है जो कि अब तक किसी ऐसे सार्वजनिक शौचालय के दरवाजे के भीतर की तरफ ही हासिल होती थी। उसमें भी पहले और बाद में उसी शौचालय में जाने वाले लोग तो यह अंदाज लगा ही सकते थे कि यह किसने लिखा होगा, लेकिन इंटरनेट पर जहां भारत के ही करोड़ों लोग हैं, और जहां बेचेहरा बने रहने की पूरी सहूलियत हासिल है वहां पर पखाने की इस दरवाजे के भीतर लिखने वाले का अंदाज भी लगाना मुमकिन नहीं है। कहने को तो यह भी है कि कंप्यूटर, इंटरनेट और फोन पर भेजा गया एक शब्द भी इतनी जानकारियों के साथ दर्ज होता है कि उसे तलाश कर अदालत में साबित किया जा सकता है। लेकिन एक सवाल यह उठता है कि कोलकाता के बॉटनिकल गार्डन के बिना ओर-छोर के अंतहीन फैले हुए बरगद के पेड़ पर टहलती हुई लाखों चीटियों में से किसी एक चींटी को कैसे तो कोई तलाशेगा और फिर कैसे उसके पदचिन्ह अदालत में साबित करेगा? कैसे कोई समंदर में रेत के एक कण को पहचानकर उसे कानून के कटघरे तक ले जाएगा? यह काम डॉन को पकडऩे से भी मुश्किल है।
दूसरी बात यह कि अभिव्यक्ति की जिस स्वतंत्रता को लेकर कानून अपने आपमें अभी कमजोर है, एक-एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट तक बहस गई हुई है, ऐसे में करोड़ों लोगों की रोजाना की अभिव्यक्ति को पुलिस या कोई दूसरी जांच एजेंसी कब तक पकड़ते रहेगी और अदालतों में लगी हुई मामलों की कतारों में ऐसे मामलों को कब जगह मिलेगी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरे लोगों के अपने सम्मान, अपने निजी जीवन के हक, एक की धार्मिक भावनाएं और दूसरे की धार्मिक भावनाएं, एक के नैतिक मूल्य और दूसरे के नैतिक मूल्य, इन सबमें इतने किस्म की विविधता है, टकराव है कि कोई भी दूसरे की कही हुई बात को अपना अपमान मान सकते हैं, और अपने हक का दावा कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो कहने वाले लोग हैं, लिखने और इंटरनेट पर डालने वाले लोग हैं उनके अपने ये तर्क हो सकते हैं कि अभिव्यक्ति की यह उनकी अपनी स्वतंत्रता है।
कहने के लिए भारत का मौजूदा, और नया भी, सूचना तकनीक कानून इतना कड़ा है कि वह लोगों को छपी हुई बातों के मुकाबले, इंटरनेट पर डाली गई बातों के लिए अधिक आसानी से अधिक कड़ी सजा दिला सकता है। लेकिन सवाल यह है कि पहले से बोझ तले टूटी कमर वाली जांच एजेंसियों और अदालतों के पास ऐसे नए मामलों के लिए वक्त कहां से निकलेगा? कहने के लिए सरकार के पास पानी की जांच करने के लिए सहूलियत है, लेकिन अगर देश भर के हर नदी-तालाब के पानी की जांच हर हफ्ते करवाई जाए तो क्या इन प्रयोगशालाओं से कोई नतीजे निकल सकेंगे? इसलिए हम इस मौजूदा हाल को किसी आसान इलाज के लायक नहीं समझते। हम यहां पर अपनी तरफ से कोई बात इसलिए सुझाना नहीं चाहते क्योंकि दुनिया के लोगों की अभिव्यक्ति की जरूरतें अलग-अलग हैं। हमें तो आए दिन, या रोज-रोज लिखने का मौका मिल जाता है, जिन लोगों को तकलीफ हमसे ज्यादा है और कहने को जगह कहीं नहीं हैं, वे लोग अपनी भड़ास को, अपनी शिकायत या तकलीफ को अगर इंटरनेट पर नहीं निकालेंगे तो वह भड़ास उनके मन के भीतर इक_ा हो-होकर किसी अलग किस्म का धमाका करेगी।
यहां पर लगे हाथों हम भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एक और पहलू पर भी बात करना चाहेंगे। यहां सेंसर हो चुकी फिल्में के पर्दे पर पहुंचने के पहले ही उनके खिलाफ अदालतों में मामले दर्ज होने लगते हैं, किसी की तस्वीर को लेकर मामला चलने लगता है तो किसी गाने को हटाने की मांग होने लगती है। धर्मों को लेकर सामाजिक तनाव इतना है कि खुलकर उस बारे में बात नहीं हो सकती और एक बहुत ही सतही जुर्म की तरह, एक थाने के स्तर पर ही किसी के लिखे के खिलाफ, किसी के कहे के खिलाफ यह जुर्म दर्ज हो जाता है कि उसने किसी और की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाई है। हजारों ईश्वरों वाले भारत जैसे देश में किसी एक के धार्मिक अधिकार भी किसी दूसरे की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने वाले हो सकते हैं। एक धर्म पूरी तरह अहिंसा पर चलता है और उसके लोग यह दावा कर सकते हैं कि दूसरे धर्म के लोग जब बलि या कुर्बानी देते हैं, तो अहिंसा की उनकी धार्मिक भावना को चोट पहुंचती है। किसी धर्म या आध्यात्म के तहत महिलाओं से भेदभाव की व्यवस्था हो सकती है, और कोई दूसरा धर्म यह कह सकता है कि उनके देश में ऐसा भेदभाव उनकी धार्मिक भावना को आहत करता है। आज योरप के कई देशों में यह हो भी रहा है। मुस्लिम महिलाओं के बुर्के के खिलाफ फ्रांस और कुछ दूसरी जगहों पर जिस तरह के कानून बन रहे हैं उन्हें मुस्लिम अपने धार्मिक अधिकारों के खिलाफ मान रहे हैं और दूसरे लोग उसे अपने देश की संस्कृति के खिलाफ मान रहे हैं। तो ऐसे टकराव इंटरनेट के बिना भी चलते हैं जहां पर कि लोगों के चेहरे हैं, उनकी शिनाख्त है।
भारत के मौजूदा हाल में हमें कुछ बहुत ही खतरनाक किस्म की साम्प्रदायिक या आतंकी बातों के अलावा, इंटरनेट पर अधिक रोक-थाम की गुंजाइश इसलिए नहीं दिखती क्योंकि इस बात पर मतभेद बने रहेगा कि क्या आपत्तिजनक है, और क्या नहीं। लेकिन भारत की सरकार ने और एक अदालत ने यह बात इंटरनेट कंपनियों से कही है, और अब करोड़ों लोग उत्सुकता से यह देख रहे हैं कि आपत्तिजनक और अभिव्यक्ति की कौन सी परिभाषाएं लागू होती हैं। दुनिया का अब तक का अनुभव तो यह रहा है कि कुछ बहुत हिंसक, बहुत आतंकी और बच्चों के सेक्स-शोषण जैसे जाहिर तौर पर पहचाने जा सकने जुर्म तो एजेंसियों के घेरे में आ जाते हैं लेकिन छोटी-मोटी गाली-गलौज और छोटा-मोटा चरित्र हनन रोकने के लायक माना नहीं जाता। लायक न मानने के यहां पर हमारे दो मतलब हैं, एक तो यह कि उन्हें इतनी अहमियत नहीं दी जाती कि उसे रोकने की कोशिश हो, दूसरी बात यह कि उसे रोकना कानूनी-तकनीकी रूप से मुमकिन ही न हो।
भारत में जो लोग आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मजा लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि हजार बरस पहले हिन्दुओं की बनाई नग्न प्रतिमाओं की तरह की कुछ पेंटिंग्स बनाने की वजह से मकबूल फिदा हुसैन को इस किस्म के इतने कानूनी मुकदमे झेलने पड़े कि बची जिंदगी सैकड़ों अदालतों में फेरे लगाने के बजाय उन्होंने इस देश को ही छोड़ देना बेहतर समझा। उन्हें तो दुनिया के कई देशों में जगह मिल गई, लेकिन बाकी लोगों की कही छोटी-छोटी बातों पर भी अगर उन्हें अदालतों में इस तरह खड़ा कर दिया जाएगा तो वे कैसे जिंदा रह पाएंगे? और यह काम बहुत मुश्किल भी नहीं है। अपनी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने के तर्क के साथ ही लोग अगर देश भर की हर जिला अदालत में किसी एक के खिलाफ मामले दर्ज करेंगे तो अब कोई कितने जिलों में हर पेशी पर जा पाएगा? हम किसी भी नए कानून के बनाए जाने के पहले मौजूदा कानूनों पर अमल की नाकामयाबी पर सोच-विचार बेहतर समझते हैं। बहुत से ऐसे मामले रहते हैं जिनमें आज के कानून का इस्तेमाल न कर पाने वाले नालायक लोग नए कानूनों को बनाने की बात करते हैं ताकि उनकी आज की कमजोरियां, आज के कानून की कमजोरियां साबित की जा सकें।
इंटरनेट पर लोगों की लिखने की आजादी अब एक ऐसी हकीकत है जो वापिस नहीं जा सकती। एक संभावना ने जन्म जब ले लिया, तो फिर उसे मां के पेट में डाला नहीं जा सकता। अब वह कितनी अच्छी है और कितनी बुरी, उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाए और कैसे निपटा जाए, यही बात हो सकती है और सच तो यह है कि आज इंटरनेट बिना किसी मां-बाप के, बिना किसी पालने वाले के, अपने आप पलने वाला माध्यम बन चुका है और उस पर नामुमकिन रोक-टोक की कोशिश भारत की आज की सरकार को ऐसा बताती है मानो उसके पास लुकाने-छुपाने को बहुत कुछ है।
हमारा यह मानना है कि इंटरनेट पर हमले उन्हीं लोगों पर होते हैं जो जिंदगी में कुछ बने हुए हैं। ऐसे लोग वहां पर झूठ का पर्दाफाश कर सकते हैं बजाय अदालतों के। लेकिन कुछ मामलों में अगर बदनीयत हमलावर, कानून तोड़ते हुए कुछ लिखते हैं, तो वे अपनी मुसीबत का सामान खड़ा कर रहे हैं। अधिकार और जिम्मेदारी को मिला-जुलाकर ही देखा जा सकता है और ऐसा कुछ भी करते हुए हुसैन को याद रखना चाहिए जो अपने वतन लौटने के बजाय परदेस में ही गुजर गए, हिंदुस्तानी जेल के बजाय। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
सोशल मीडिया पर एक लाइन अभी पढऩे मिली कि एक दुख भरी शादी के मुकाबले बिना दुख वाला तलाक बेहतर होता है। बात एकदम खरी है और उन देशों या समाजों के लिए इसकी अधिक अहमियत है जहां पर तलाक को एक बदनाम शब्द माना जाता है। हम यहां पर ऐसे समाज के तलाक की चर्चा नहीं कर रहे जहां मर्दों को ही इसका आसान हक हासिल और औरतों को यह हक मानो मिला हुआ नहीं है, तमाम लोगों की बात कर रहे हैं, जहां पर तलाक देना दोनों के ही हक की बात होती है. वहां पर एक तकलीफ और यातना भरी हुई शादीशुदा जिंदगी को ढोने के बजाय उससे आजाद होकर अकेले होना और फिर आगे की अपनी जिंदगी को खुद तय करना किस तरह बेहतर होता है इसे समझने की जरूरत है।
हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से में जब शादी के बाद लडक़ी को घर से विदा किया जाता है तो उसे रवानगी के तोहफे की शक्ल में एक नसीहत दी जाती है कि डोली मां-बाप के घर से उठ रही है, अब अर्थी ससुराल से उठना चाहिए। इसे एक अच्छी महिला होने का पैमाना माना जाता है कि वह ससुराल में मर-खप जाए, तकलीफ की जिंदगी गुजार ले, या तनाव को बर्दाश्त कर ले, लेकिन उसे छोडक़र कभी ना निकले। बहुत से भाई इस बात के हिमायती अधिक दूर तक होंगे कि लडक़ी लौटकर मां बाप के घर कभी ना आए क्योंकि मां-बाप तो अपना वक्त गुजार कर रवानगी डाल देंगे, और उसके बाद लौटी हुई बहन भाइयों की ही जिम्मेदारी रह जाएगी। उसके बाद उस बहन के अगर बच्चे हुए तो उनकी भी जिम्मेदारी भाइयों के परिवार पर आएगी, और कानून की अगर बात करें तो लडक़ी मां-बाप की दौलत में बराबरी की हकदार भी होती है, इसलिए भी हो सकता है कि भाइयों में बहन के लौटने के नाम से ही दहशत होने लगे। ऐसे में हिंदुस्तान के अधिकतर समाज में लडक़ी से ससुराल की ज्यादतियां बर्दाश्त करने की उम्मीद की जाती है। चाहे वह यातना झेलते-झेलते मानसिक रोगी ही क्यों न हो जाये, वह खुदकुशी ही क्यों न कर ले, या उसकी दहेज हत्या ही क्यों ना हो जाए. आमतौर पर लडक़ी के मां-बाप, उसके भाई इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि वह किसी तरह ससुराल में एडजस्ट हो जाए, वहां उसका तालमेल बैठ जाए।
लेकिन जब हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं और एक नजरी सर्वे सा करते हैं कि कौन सी लड़कियां ऐसी हैं जो तनाव को बाकी जिंदगी झेलने के बजाय, एक सीमा तक झेलने के बाद ससुराल और शादी के बंधन से निकलने की हिम्मत जुटा पाती हैं? ऐसा सोचने पर आसपास दिखता यह है कि या तो बहुत संपन्न परिवारों की ऐसी लड़कियां जिनके मां-बाप, भाई उनके साथ में खड़े हुए हैं, वे बाहर निकलने का हौसला जुटा पाती हैं, या फिर मजदूर तबके की ऐसी महिलाएं जिन्हें घर लौटने के बाद में एक कोठरी में अपनी कमाई पर जीने की हिम्मत रहती है, वह भी शादी को तोडक़र बाहर निकलने की हिम्मत दिखा पाती हैं। लेकिन इनसे परे तलाक के मामलों में बाकी महिलाओं का हौसला कुछ कम दिखाई पड़ता है, और केवल वही महिलाएं तलाक का हौसला कर पाती हैं, जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहती हैं. यह निष्कर्ष किसी सर्वे पर आधारित नहीं है केवल आसपास के मामलों को देखते हुए ऐसा लगता है कि आर्थिक रूप से संपन्न महिला यातना के सिलसिले को तोडऩे का हौसला जुटा पाती है। इसलिए यह बात बहुत मायने रखती है कि शादी के पहले ही हर लडक़ी को आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाए ताकि उसके मायके के लोग अगर उसका साथ न भी दें तो भी वह अपने दम पर जिंदा रह सके।
अपने दम पर जिंदा रह सके यह बात तो सोचने का मतलब किसी कोने से भी यह सुझाना नहीं है कि शादी के बाद लडक़ी को उसके मायके की संपत्ति में हिस्सा ना मिले या तलाक के बाद उसके पति और ससुराल से उसे बराबरी की एक जिंदगी जीने का इंतजाम ना मिले। हम इन दोनों इंतजामों के साथ-साथ यह बात सुझाना चाहते हैं कि हर लडक़ी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना उसके परिवार और समाज इन दोनों के लिए भी जरूरी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसी सरकारें जो कि गरीब लड़कियों की शादी में सरकार की तरफ से समारोह का इंतजाम करती हैं, और घर बसाने के लिए कुछ सामानों का तोहफा भी देती हैं, उन्हें ऐसे लुभावने रस्म-रिवाज का जिम्मा उठाने के बजाय महिलाओं की आत्मनिर्भरता के बारे में कुछ अधिक सोचना चाहिए, और करना चाहिए। सोचने की जरूरत है कि किसी वजह से कोई लडक़ी या महिला अकेले रह जाए, तो उसकी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए सरकार क्या कर सकती है?
हिंदुस्तान के ही केरल जैसे प्रदेश को देखें तो वहां ना केवल पढ़ाई-लिखाई बल्कि कई किस्म की पेशेवर ट्रेनिंग का ऐसा इंतजाम है कि केरल के कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रह जाते। पूरे हिंदुस्तान में मेडिकल ढांचे में जितने किस्म के तकनीकी काम रहते हैं, उनमें केरल से निकले हुए लोग बड़ी संख्या में दिखते हैं। उनके अलावा अंग्रेजी का डिक्टेशन लेने या अंग्रेजी टाइप करने जैसे कामों के लिए भी केरल के लोग बहुत दिखते हैं। फिर बड़ी-बड़ी मशीनों को चलाने में दिखते हैं, उनकी मरम्मत में दिखते हैं। जहां पर पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ हुनर सिखाने का इंतजाम भी होता है, वहां सभी लोग आत्मनिर्भर हो जाते हैं। हमारा यह मानना है कि एक आत्मनिर्भर समाज ही आत्मसम्मान से भरा हुआ समाज हो सकता है, और ऐसा ही समाज यातनामुक्त भी हो सकता है, क्योंकि वहां लोग मजबूरी के संबंधों को ढोने के बजाय बाहर निकलकर अपने दम पर जीने की एक संभावना तो देखते ही हैं।
हिंदुस्तान में शादी को लेकर जितने किस्म का पाखंड प्रचलन में है, वह बताता है कि कन्या का दान किया जाता है। हिंदू शादी में इस्तेमाल होने वाला यह शब्द मानो लडक़ी का दर्जा जिंदगी भर के लिए तय कर देता है कि वह दान में दी जाने वाली एक चीज है। और जिसे दान में कोई सामान मिलता है, उसे उस सामान का अधिक महत्व तो कभी समझ में आता भी नहीं है। इसके साथ-साथ हिंदू समाज में पति के जितने प्रतीकों को सुहाग के प्रतीकों के नाम पर एक महिला पर लाद दिया जाता है, उससे भी वह एक आश्रित का दर्जा पा लेती है, और उसका आत्मविश्वास, उसकी आत्मनिर्भरता इन सब को अच्छी तरह कुचल दिया जाता है। फिर समाज की मान्यताएं भी रहती हैं कि औरत के सुहागिन होकर मरने को उसकी किस्मत की बात माना जाता है। मतलब यह कि औरत अपने पति की मरते तक सेवा करें और उसके मरने के साथ ही उसके प्रतीकों को उतार हिंदुस्तान में शादी को लेकर जितने किस्म का पाखंड प्रचलन में है कामा वह बताता है की कन्या का दान किया जाता है। हिंदू शादी में इस्तेमाल होने वाला यह शब्द मानव लडक़ी का दर्जा जिंदगी भर के लिए तय कर देता है कि वह दान में दी जाने वाली एक चीज है। और जिसे दान में कोई सामान मिलता है उसे उस सामान का अधिक महत्व तो कभी समझ में आता भी नहीं है। इसके साथ साथ हिंदू समाज में पति के जितने प्रतीकों को सुहाग के प्रतीकों के नाम पर एक महिला पर ला दिया जाता है उससे भी वह एक आश्रित का दर्जा पा लेती है और उसका आत्मविश्वास उसकी आत्मनिर्भरता इन सब को अच्छी तरह कुचल दिया जाता है। फिर समाज की मान्यताएं सी रहती हैं की औरत के सुहागिन होकर मरने को उसकी किस्मत की बात मानी जाती है। मतलब यह की औरत अपने पति कि मरते तक सेवा करें और उसके मरने के साथ है ही उसके प्रतीकों को उतार दे, तोड़ दे, और पोंछ दे।
एक महिला के दिमाग में यह बैठा दिया जाता है कि शादी सात जन्मों का संबंध रहता है। इसलिए वह एक जन्म के बाद भी इस बंधन से आजाद होने की नहीं सोच पाती। ऐसी मानसिकता के बीच जरा भी हैरानी की बात नहीं रहती कि कोई महिला पूरी जिंदगी शादीशुदा जिंदगी की यातनाओं को ढोते हुए मर-खप जाती है, और शायद ही कभी अपने मां-बाप के घर पर दोबारा अपना हक पाने के लिए लौट पाती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता से परे एक लडक़ी के सामाजिक और पारिवारिक का हक पर भी खुलकर बात होनी चाहिए और इस सोच को जगह-जगह कुचलना चाहिए कि मां-बाप के घर से बस डोली ही निकलती है, और अर्थी तो ससुराल से ही निकलेगी।
हिंदुस्तान के कानून में लडक़ी को मां-बाप की दौलत पर बराबरी का हक दिया गया है, और शादी के खर्च या दहेज को इस हक का विकल्प मान लेना नाजायज बात तो होगी। यह समझने की जरूरत है कि समाज में प्रचलित इस धारणा को भी जगह-जगह धिक्कारना चाहिए कि दहेज के साथ लडक़ी का हक देना पूरा हो जाता है। मां-बाप लडक़ी की शादी पर खर्च अपनी शान शौकत के लिए करते हैं। और दहेज लेना-देना तो वैसे भी जुर्म के दर्जे में आता है और इस सिलसिले को खत्म करना जरूरी है। कोरोना और लॉकडाउन के पूरे दौर में शादियों में 25-50 लोगों का ही बंधन रहा, और वैसे में भी लोगों ने शादियां कर दीं, समारोह कर दिए।
इसलिए अब एक कानून बनाकर प्रदेश सरकारों को भी अतिथि नियंत्रण लागू करना चाहिए ताकि लड़कियों के मां-बाप पर दिखावे की शान-शौकत का जलसा करने का बोझ भी ना रहे। ऐसा करके कानून एक ऐसा माहौल खड़ा करने में मदद कर सकता है जिसमें लड़कियों के नाम पर खर्च दिखाने के लिए शानशौकत की दावत दर्ज कर ली जाए, जिनसे उस लडक़ी को अपनी किसी मुसीबत के वक्त कोई मदद तो मिलती नहीं है। इसलिए लडक़ी के हक और उसकी आत्मनिर्भरता के मुद्दे पर समाज में व्यापक चर्चा जरूरी है, अलग-अलग कई मंचों पर इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, और ऐसी बात जब अधिक होती है तो वह नीचे तक भी उतरती है. सामाजिक मंचों को ऐसी बहस छेडऩी चाहिए ताकि लोगों के दिल-दिमाग में बैठे हुए पुराने ख्यालात निकल भी सकें, और नई कानूनी बातें घुस भी सकें।
हिंदुस्तान जैसे समाज में लडक़ी और महिला की आर्थिक आत्मनिर्भरता को उनके बुनियादी मानवाधिकार मानना चाहिए। और उनकी ऐसी आत्मनिर्भरता उनके बच्चों की परवरिश के लिए भी एक बेहतर नौबत रहती है, जब बच्चे रिश्तेदारों से किसी मदद के मोहताज नहीं रहते, और अपनी मां की कमाई पर अच्छे से जिंदा रह सकते हैं. ऐसा समाज ही एक बेहतर समाज भी बन सकता है जिसमें एक महिला आर्थिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर हो, और आत्मविश्वास से भरी हुई हो।
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिल्ली प्रवास की खबर से राजनीति में गर्मी आ गई है कि क्या वे अगले चुनाव को लेकर अपने आपको एक सर्वमान्य विपक्षी नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं? और ऐसी अटकलबाजी के पीछे, अभी हाल में ही तृणमूल कांग्रेस के शहीदी दिवस की रैली में ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से गैर एनडीए विपक्षी दलों को एक होने का आह्वान किया था और कहा था कि अब कुल ढाई-तीन बरस बाकी हैं, और लोग अगर भाजपा को हटाना चाहते हैं तो उन्हें गठबंधन बनाकर साथ में काम करना चाहिए। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी पर हमला करते हुए कहा था कि यह सरकार देश में एक निगरानी राज बनाना चाह रही है। यह बात पेगासस नाम के निगरानी सॉफ्टवेयर को लेकर उन्होंने कही, और निगरानी की ऐसी बातें भाजपा के कुछ बंगाल के नेता भी पिछले दिनों कह गए हैं, जिसमें एक नेता ने सार्वजनिक रूप से एक पुलिस अधीक्षक को धमकी दी कि वह किससे बात करते हैं उसके पूरे कॉल डिटेल्स उनके पास मौजूद हैं, और वह आईपीएस अफसर हैं, और क्या वह कश्मीर तबादला चाहते हैं? बंगाल के बहुत से नेताओं के साथ दिक्कत यह है कि वे जुबानी हमले करते हुए यह नहीं समझ पाते कि उनकी कही हुई बातें कैसे उनके ही लिए आत्मघाती साबित होंगी, क्योंकि ऐसी सार्वजनिक धमकी देकर इस नेता ने खुद ही को एक पुलिस जांच में उलझा लिया है। खैर हम यहां पर बंगाल की राजनीति पर अधिक बात करना नहीं चाहते क्योंकि हम राष्ट्रीय स्तर पर ममता की संभावनाओं पर बात करना चाहते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर ममता से परे की संभावनाओं पर भी।
दरअसल कुछ दिन पहले जब ममता बनर्जी के विधानसभा चुनाव तक के रणनीतिकार प्रशांत किशोर मुंबई जाकर दो बार शरद पवार से मिले, और उसके बाद दिल्ली आकर 10 जनपथ में उन्होंने जिस तरह से सोनिया, राहुल, और प्रियंका, इन सबसे मुलाकात की, उससे भी ये अटकलें आगे बढ़ीं कि क्या वे भाजपा के खिलाफ देश में कई पार्टियों के मोर्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं? और सच तो यही है कि आज जब कभी इस देश में लोग मोदी सरकार से थककर, या नाराज होकर, उसे हटाने के बारे में बात करते हैं, तो पहला सवाल यही खड़ा होता है कि मोदी का विकल्प कौन है? भारत की राजनीति में इसे टीना फैक्टर कहते हैं, टीना का मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव। अब बात एक किस्म से सही भी है कि मोदी ने पिछले करीब 10 बरस में अपने आपको इस देश का ‘एक सबसे बड़ा’ नेता साबित करते हुए, अपने आपको ‘सबसे बड़ा नेता’ स्थापित कर दिया है। हम इसे इतिहास में मोदी की जगह नहीं बता रहे हैं, बल्कि आज की भारतीय चुनावी राजनीति में मोदी की स्थिति को बयान कर रहे हैं।
मोदी के बारे में उनके आलोचक भी जब मूल्यांकन करने बैठते हैं, और इतिहास में मूल्यांकन नहीं, आने वाले अगले आम चुनाव में उनकी चुनावी संभावनाओं के मूल्यांकन में, तो उन्हें भी लगता है कि मोदी जैसा कोई नहीं। उनमें से कुछ लोग लिखते भी हैं कि मोदी को खुद मोदी ही हरा सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जनसंघ से लेकर भाजपा के इतिहास तक के सबसे बड़े नेता रहे अटल बिहारी वाजपेई ने मोदी की गुजरात सरकार को राजधर्म का पालन न करने वाली सरकार माना था, उसके बाद भी मोदी पार्टी के भीतर के मोर्चे पर जीते, और उसके बाद गुजरात में उन्होंने दो-दो चुनाव जीते। इसलिए मोदी को लेकर जल्दी में कोई मूल्यांकन करना गलत होगा क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं हुआ है जिसने चुनाव जीतने की मशीन चलाने में ऐसी महारत हासिल की हो। बल्कि यह मशीन भी मोदी की ही बनाई हुई है, जो जानते हैं कि किस तरह भारत में मतदान के दिन भारत के चुनाव आयोग की नजरों और उसके काबू से परे जाकर नेपाल और बांग्लादेश में दिन भर मंदिरों का दौरा करके भी टीवी स्क्रीन के मार्फत हिंदुस्तान में चुनाव प्रचार किया जा सकता है। इसलिए यह बात अपने आपमें सही है कि चुनाव प्रचार के मामले में मोदी जैसा अब तक न कोई था, और न आज कोई है।
जब मोदी के विकल्प के बारे में सोचा जाए तो जो चेहरे सामने दिखते हैं वहीं से बात हो सकती है, ममता बनर्जी ने जिस अंदाज में बंगाल का चुनाव लड़ा और मोदी और शाह की टीम को बुरी शिकस्त दी, उनके सारे दावों को गलत साबित किया, उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, तो बंगाल के चुनावी नतीजे आने के साथ-साथ ममता की राष्ट्रीय संभावनाओं के बारे में भी चर्चा शुरू होनी थी। वह चर्चा श्रद्धांजलि और अभिनंदन के मंचों से की जाने वाले विशेषण से भरी चर्चा की हद तक तो शुरू हुई, लेकिन फिर लोगों को शायद उसमें कोई दम नहीं दिखा। ममता बनर्जी जिस तरह बंगाल की राजनीति में कांग्रेस और वामपंथियों दोनों को बुलडोजर से कुचल चुकी हैं, उसके बाद सवाल यह भी उठता है कि ये दोनों पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी को कितना बड़ा नेता बनाना चाहेंगी? और फिर वामपंथी तो ऐसे हैं जिनके पास केरल, बंगाल और त्रिपुरा जैसे गिने-चुने तीन राज्य ही थे, और अगर वामपंथियों की कोई संभावना केरल के बाद बचेगी तो हो सकता है कि उसमें बंगाल को वे गिनकर चल रहे हों, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विरोध करने के लिए भी वामपंथी ममता बनर्जी के साथ किसी एक गठबंधन में आएंगे ऐसा मुमकिन नहीं दिखता है।
दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार जाहिर तौर पर देश के सबसे बुजुर्ग, और शायद सबसे वरिष्ठ भी, गैर भाजपाई, गैर एनडीए नेता हैं, और उनके बारे में भी ऐसी चर्चा चलती है कि वे मोदी के मुकाबले एक गठबंधन के मुखिया हो सकते हैं। लेकिन मतदाताओं के दिल को रिझाने वाली बातों को देखें तो शरद पवार के साथ भी दिक्कत यह है कि महाराष्ट्र और दिल्ली से परे आम जनता में उनका असर सीमित है। वे ममता के मुकाबले कुछ बेहतर हिंदी भाषी जरूर हैं, लेकिन हिंदी भाषण देना उनकी खूबी में कहीं नहीं है। यही दिक्कत ममता बनर्जी के साथ भी है। इसलिए मोदी के तेजाबी और जलते-सुलगते चुनावी भाषणों के मुकाबले ये दोनों नेता किसी किनारे भी नहीं टिक पाएंगे, इस बात को भूलना नहीं चाहिए।
अब बहुत से लोगों को यह लगता है कि भाजपा के अलावा कांग्रेसी एक ऐसी पार्टी है जो आज की अपनी दुर्गति में भी देश में सबसे अधिक फैली हुई पार्टी है, जिसका हर प्रदेश में अस्तित्व अभी भी बाकी है। हो सकता है कि बंगाल की तरह और राज्य भी हों जहां पर कांग्रेस का कोई भी विधायक न बचा हो, लेकिन उससे पार्टी संगठन खत्म नहीं हो पाया है और कांग्रेस एक पार्टी के रूप में अभी भी बची हुई है। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आज जो अनिश्चितता बनी हुई है, वह कांग्रेस की संभावनाओं पर भारी पड़ रही है। राहुल गांधी में जो लोग मोदी के मुकाबले एक चेहरा देखते हैं, उनको यह समझने में दिक्कत होती है कि अभी तो राहुल गांधी के अगला कांग्रेस अध्यक्ष बनने का भी ठिकाना नहीं है, और हो सकता है कि कांग्रेस के जो दो दर्जन बड़े नेता बागी तेवरों के साथ संगठन चुनाव की मांग कर रहे थे, उनमें से बहुत से लोग राहुल गांधी की फिर से अगुवाई के हिमायती ना हों। ऐसी हालत में राष्ट्रीय स्तर पर यूपीए जैसे किसी गठबंधन का नेता बनने के पहले कांग्रेस के भीतर कांग्रेस का नेता तय होने की जरूरत रहेगी। इसलिए राहुल गांधी के बारे में मोदी के मुकाबले किसी संभावना को देखना उसी वक्त हो पाएगा जिस वक्त कांग्रेस के भीतर उनकी संभावनाएं औपचारिक रूप से तय और घोषित हो जाएं।
देश की जिन पार्टियों को मोदी के विकल्प के रूप में एक गठबंधन या एक नेता को तय करने के लिए अभी सही समय लग रहा है, उनकी सोच गलत नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है जब पहले एक गठबंधन बना हो उसने चुनाव जीता हो, चुनाव मुद्दों पर लड़ा और जीता गया हो, चुनाव तानाशाही के खिलाफ लड़ा गया हो और जीता गया हो, चुनाव सेंसरशिप या मनमानी या जुल्म के खिलाफ लडक़र जीता गया हो, और प्रधानमंत्री उसके बाद तय किया गया हो। हिंदुस्तान की राजनीति में चार से ज्यादा प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिनके प्रधानमंत्री बनने के ठीक पहले तक कोई उनके बारे में अंदाज नहीं लगा सकते थे कि वे प्रधानमंत्री बनेंगे। चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल, देवेगौड़ा, नरसिंह राव, और मनमोहन सिंह। अपने वक्त में इन सभी की संभावनाएं कभी ऐसी मजबूत नहीं थीं कि इनकी अगुवाई में कोई चुनाव लडक़र, इनके चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करके, कोई चुनाव जीता जा सकता था। लेकिन वक्त ऐसा आया कि इनमें से हर कोई प्रधानमंत्री बने, और मनमोहन सिंह तो दो-दो बार प्रधानमंत्री बने।
इसलिए हम आज राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के मुकाबले किसी चेहरे के तय होने को लेकर बहुत निराश नहीं हैं, और न ही हमें ममता बनर्जी की कोशिश या उनकी तरफ से प्रशांत किशोर की कोशिश अपरिपच् लग रही है कि अभी उसका समय नहीं आया है। ना सिर्फ अगला चुनाव लडऩे के लिए या कि प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐसा गठबंधन होना चाहिए, बल्कि आज देश के सामने जो बहुत से खतरे खड़े हुए हैं, उनसे जूझने के लिए भी ऐसे गठबंधन की जरूरत है, और हो सकता है कि ऐसा कोई औपचारिक गठबंधन न भी बने लेकिन गैरभाजपा गैरएनडीए पार्टियों के बीच एक व्यापक तालमेल बनकर बात आगे बढ़ सके। ऐसे किसी तालमेल की जरूरत आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी गैरभाजपाई दलों को पड़ सकती है जहाँ अभी तक के माहौल में ऐसे किसी तालमेल की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसलिए ममता बनर्जी या शरद पवार की पहल हो सकता है भारतीय लोकतंत्र में एक मजबूत मोर्चे के रूप में मुद्दों को लेकर अगले ढाई बरस लडऩे के काम आए, और उसके बाद के चुनाव में काम आए या ना आए यह एक अलग बात रहेगी। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
सोशल मीडिया पर हर दिन कई समझदार दिखते लोगों का लिखा हुआ पढऩे मिलता है जिसमें इंसान की घटिया हरकतों, इंसान के तरह-तरह के जुर्म में इनको कोसने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं भेड़ की खाल ओढ़े हुए भेडि़ए का जिक्र होता है, तो कहीं आस्तीन के सांप का, तो कहीं रंगे सियार की बात होती है, तो कहीं घडिय़ाल के आंसुओं की। जानवरों के बारे में बड़ी मामूली सी जानकारी रखने वाले भी इस बात को जानते हैं कि इंसान अपनी खुद की कमीनगी को जानवरों की कुछ एक काल्पनिक खामियों के साथ जोडक़र मानो अपने पर लगी तोहमत को घटाना चाहते हैं।
अब इंसानों के किए हुए कामों को देखें तो लगता है कि जानवरों में भला कौन हैं जो ऐसे काम करते हैं? एक भी मिसाल जानवरों में ऐसी नहीं मिल सकती जो इंसानों की कमीनगी का मुकाबला कर सके। अब आज की एक खबर है कि उत्तर भारत के किसी एक गांव में एक बाप-बेटी खुले खेत में सेक्स कर रहे थे और लोगों ने घेरकर उनका वीडियो बनाया, उन्हें वहां से भगाया तो वह लोगों पर पथराव करने लगे। अब उनकी हिफाजत के लिए गांव में उनके घर के बाहर पुलिस तैनात की गई है वरना यह खतरा है कि गांव के लोग उन पर हमला कर सकते हैं। कल या परसों एक दूसरी खबर थी कि एक बेटे ने अपनी मां को मारकर उसकी किडनी और अंतडिय़ाँ बाहर निकाल लीं। अखबार में बैठे हुए यह भी समझ नहीं पड़ता कि इस तरह की हिंसा या इस तरह के जुर्म की कितनी खबरें छापी जाएं, उन खबरों में कितना खुलासा किया जाए। क्या उससे समाज को सावधान होने का मौका मिलेगा या इन खबरों का ही समाज पर बुरा असर पड़ेगा, यह तय करने में मुश्किल होने लगती है। जानवरों में कौन से ऐसे हैं जिनमें इस तरह की मिसालें मिल सकें?
इंसान कैसा-कैसा करते हैं, इसकी एक मिसाल कुछ सौ बरस पहले की अभी पढऩे मिली जब कोरोना से बचाव के लिए टीकों की खबर के साथ-साथ वैक्सीन के इतिहास पर भी छपा, और पढऩे मिला। इतिहास का ऐसा ही एक पन्ना 1803 के बरस का है जब दुनिया भर में स्मॉलपॉक्स बहुत बुरी तरह फैला हुआ था, और वह लोगों को बड़ी संख्या में मार भी रहा था, साथ-साथ उनके बदन पर गहरे दाग छोड़ रहा था, कई लोगों की आंखें खराब कर दे रहा था। वैसे में 1796 के आसपास एक ब्रिटिश डॉक्टर ने स्मालपॉक्स के संक्रमण से बचाव की एक तरकीब ढूंढी, और उसने यह पाया कि एक दूसरा संक्रमण कॉउपॉक्स ऐसा है जिससे संक्रमित लोगों को स्मालपॉक्स नहीं हो रहा था। उसने लोगों को स्मालपॉक्स संक्रमण से बचाने के लिए कॉउपॉक्स के वायरस देने शुरू किए, और ऐसे दुनिया की पहली वैक्सीन सामने आई।
इसका तरीका भी बड़ा आसान था, जिन लोगों को कॉउपॉक्स से संक्रमित किया जाता था, उनके बदन पर 9-10 दिनों में कुछ फोड़े हो जाते थे, और दूसरे लोगों के बदन में खरोंच लगाकर उन फोड़ों का पानी निकाल कर उन्हें छुआ दिया जाता था, तो वे लोग भी कॉउपॉक्स से संक्रमित हो जाते थे, लेकिन स्मालपॉक्स के संक्रमण से बच जाते थे जो कि जानलेवा और बहुत अधिक खतरनाक संक्रमण था।
अब इसमें दिक्कत यह आ रही थी कि संक्रमित लोगों के फोड़ों से निकलने वाला पानी बहुत दूर तक नहीं ले जाया जा सकता था। उसे कुछ सौ किलोमीटर ले जाते हुए भी उसका असर खत्म हो जाता था। ऐसे में यूरोप से अमेरिका अगर यह संक्रमण ले जाना हो ताकि अमेरिका में बुरी तरह फैले हुए स्मालपॉक्स का संक्रमण रोका जा सके, तो उसकी कोई तरकीब नहीं निकल रही थी। लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है विज्ञान का एक तकनीक से रिश्ता होता है इंसानियत से नहीं, इसलिए स्पेन के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाल लिया। यह अनोखा प्रयोग था लेकिन उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया।
1803 में स्पेन के राजा की इजाजत से वहां के दो दर्जन अनाथ बच्चों को छांटकर एक जहाज पर सवार किया गया। राजा की सोच जनकल्याणकारी थी इसलिए उसने इन बच्चों के खाने-पीने का और इनके रखरखाव का अच्छा इंतजाम किया। जहाज के रवाना होने के ठीक पहले डॉक्टरों ने इनमें से दो बच्चों के शरीर में कॉउपॉक्स का संक्रमण डाल दिया। समंदर में सफर के बीच नौ-दस दिनों में इन दो बच्चों की बाहों पर लगाए गए इस टीके के जख्म फोड़ों में तब्दील हो गए और जहाज पर तैनात डॉक्टरों ने इन्हें फोडक़र इसमें से पानी निकालकर दो दूसरे बच्चों की बाहों में खरोंच लगाकर उसमें इसका संक्रमण डाल दिया। अगले नौ-दस दिनों के बाद ये दो बच्चे अपने संक्रमित फोड़ों के साथ तैयार थे, और फिर यही सिलसिला तब तक चलते रहा जब तक जहाज अमेरिका नहीं पहुंच गया। अमेरिका पहुंचने पर सिर्फ आखिरी बच्चे की बाहों में एक फोड़े में पानी था, और डॉक्टरों ने जहाज से उतरते ही उससे संक्रमित पानी निकाल कर दूसरे बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया जिन पर कि स्मालपॉक्स का खतरा दूसरी उम्र के लोगों के मुकाबले अधिक था। अब अगर देखा जाए कि ये अनाथ बच्चे बिना किसी की इजाजत के इस तरह से वैक्सीन खच्चर की तरह इस्तेमाल किए गए, और इनमें से कुछ बच्चे जहाज पर मर भी गए। तो आज वैक्सीन के कारखानों से निकलकर फ्रीजर जैसी गाडिय़ों में लदकर वैक्सीन दूर-दूर तक जाती है, और एक वक्त यह काम इन अनाथ बच्चों से करवाया गया जिन्होंने इन वैक्सीन को अपने बदन में ढोया, और अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी।
जो लोग बात-बात पर इंसान की खामियों के लिए जानवरों की मिसालें ढूंढ लेते हैं, उन लोगों को चाहिए कि इंसान की इस कमीनगी के टक्कर की कोई मिसाल जानवरों में ढूंढकर बताएं। पंछी भी हजारों किलोमीटर उडक़र कई देश पार करके हर बरस किसी एक देश पहुंचते हैं, और मौसम बदलने पर फिर वापस अपने देश आ जाते हैं, लेकिन न वे इंसानों की तरह किसी दूसरे जानवर की पीठ पर सवार होकर आते हैं, और न ही आते जाते हुए किसी दूसरे का हक का खाते हैं। इसलिए यह समझने की जरूरत है कि दुनिया के इतिहास में उसके हर दौर में इंसान जितने तरह के बुरे काम करते रहा है, उसकी कोई मिसाल इंसानों से परे कहीं देखने नहीं मिलेगी। दुनिया का इतिहास जुल्म से भरा हुआ है और हर जुल्म के लिए महज इंसान जिम्मेदार रहे हैं।
अपने आसपास के लोगों को कैदी बनाकर गुलाम बनाकर उन्हें बाजारों में नीलाम करना, उनसे जानवरों या मशीनों की तरह काम लेकर उन्हें खत्म कर देना, और उन्हें फेंक कर फिर से दूसरे गुलाम खरीद लेना ऐसे कितने ही काम बड़े आम तरीके से इंसान करते हैं।
अभी हाल के बरसों तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक जापान ने कई दूसरे देशों में अपनी फौज के लोगों के लिए वहां की स्थानीय लड़कियों और महिलाओं को रखकर चकलाघर बना दिए थे, और उनका मनचाहा शोषण करने के बाद सैनिक अपने देश लौट आए वहां पर अपनी एक अगली पीढ़ी छोडक़र। ऐसा ही अमेरिकी फौजियों ने वियतनाम में किया था, ऐसा ही तालिबान आज अफगानिस्तान में कर रहे हैं जहां वे विधवाओं और लड़कियों की लिस्ट बनाकर विधवाओं को अपने सैनिकों के हवाले कर रहे हैं ताकि वे उनका मनचाहा इस्तेमाल कर सकें। खूब बढ़-चढक़र जानवरों के खिलाफ लिखने वाले इंसानों को जानवरों में ऐसी कोई मिसाल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और नाकामयाब होने पर कम से कम आगे जानवरों के खिलाफ अपनी हैवानियत नहीं दिखानी चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)
जनसंख्या नियंत्रण हिंदुस्तान में हमेशा से एक बड़ा नाजुक मुद्दा रहा है और खासकर इमरजेंसी के दौरान देश की आबादी को काबू में लाने के लिए संजय गांधी की अगुवाई में इंदिरा सरकार ने जिस तरह की ज्यादतियां की थीं, उनसे हमेशा के लिए यह एक जुल्म की तरह देखा जाने लगा है। आज हालत यह है कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन शब्द का इस्तेमाल भी समझदार सरकारें नहीं करती हैं। लेकिन अभी जनसंख्या नियंत्रण इसलिए चर्चा में है कि भाजपा की सरकारों वाले दो प्रदेशों में जनसंख्या पर काबू पाने के लिए कुछ नियम लागू करने की तैयारी चल रही है, इनमें से एक असम है जहां पर अभी-अभी भाजपा सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में लौटी है और जिसके ऊपर चुनाव का कोई दबाव नहीं है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है जहां पर भाजपा सरकार अगले बरस चुनाव का सामना करने जा रही है और उसे एक खास राजनीतिक मकसद से अपना यह रुख दिखाना है कि वह बढ़ती हुई आबादी के खिलाफ है, और जनसंख्या को घटाने के लिए जो नियम वहां पर बनाए जा रहे हैं उन नियमों को लेकर हिंदू मतदाताओं के बीच एक धार्मिक ध्रुवीकरण की नीयत भी सरकार की दिख रही है।
इस मामले को लेकर भाजपा सरकारों के ऊपर यह साफ तोहमत लग रही है कि उसके निशाने पर मुस्लिम समुदाय है जिसमें बच्चों का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात के मुकाबले कुछ अधिक रहता है. और फिर एक बात जो मुस्लिमों के खिलाफ राजनीतिक रूप से उठती है वह यह भी रहती है कि इस समाज में एक से अधिक शादियां कानूनी हैं और हर शादी में कई बच्चे पैदा हो सकते हैं. एक लुभावना सांप्रदायिक नारा मुस्लिमों के खिलाफ यह भी चलता है कि चार बीवी और 16 बच्चे इस रफ्तार से एक दिन हिंदुस्तान में मुस्लिम ही बहुसंख्यक रह जाएंगे। जबकि आंकड़ों की हकीकत इसके खिलाफ है और मुस्लिमों के भीतर भी बड़ी रफ्तार से आबादी के बढ़ने में गिरावट आ रही है, और ऐसे आसार दिख रहे हैं कि मुस्लिम समाज में आबादी बढ़ना धीरे-धीरे राष्ट्रीय अनुपात के बराबर पहुंच जाएगा। फिर भी जब धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करना हो तो चार बीवियां और 16 बच्चे की एक संभावना या आशंका जताना एक लुभावना नारा बनता ही है।
उत्तर प्रदेश में एक शादीशुदा जोड़े के 2 बच्चों की नीति लागू करने पर बहस चल रही है और असम लागू कर चुका है। इसमें यह कहा गया है कि 2 बच्चों से अधिक बच्चे पैदा करने वाले जुड़े स्थानीय चुनावों के चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, यानी वे पंचायत और म्युनिसिपल के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है, और इस राज्य में जनसंख्या बढ़ने की दर भी देश में सबसे अधिक 2 राज्यों में से एक है, पहले नंबर पर बिहार है जहां 3.3 फ़ीसदी की जनसंख्या बढ़ोतरी है और उत्तर प्रदेश में 2.9 की जनसंख्या बढ़ोतरी है। आज देश में राष्ट्रीय जनसंख्या बढ़ोतरी 2.2 है जो कि 1950 में 5.9 थी। कुछ और आंकड़ों को देखें तो वे आंकड़े यह बताते हैं कि 1970 से 1980 के बीच के दशक में हिंदुस्तान में जनसंख्या बढ़ोतरी 2.2 से बढ़कर 2.3 से भी अधिक हो चुकी थी और दशक के आखिर तक वहीं पर बनी रही थी। यही वह दौर था जब संजय गांधी ने अपने सारे आक्रामक तानाशाह तेवरों के साथ परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया था और सड़कों पर पकड़-पकड़कर गैरशादीशुदा लोगों की भी नसें काट दी जा रही थीं। ऐसा माना जाता है कि इमरजेंसी के बाद कांग्रेस सरकार के खत्म होने और दफन होने के पीछे नसबंदी एक सबसे बड़ी वजह थी।
अब यह समझने की जरूरत है की उत्तर प्रदेश जिस अंदाज में यह जनसंख्या नियंत्रण विधेयक ला रहा है उसके तहत दो बच्चों तक सीमित रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि या मिलेंगी छुट्टियां अधिक मिलेंगी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाएंगे और किसी परिवार को रियायती राशन सिर्फ सिर्फ चार लोगों के लायक मिलेगा। दो बच्चों से अधिक के मां-बाप म्युनिसिपल और पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और ना ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे, ना ही उन्हें सरकारी सब्सिडी का फायदा मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस नई व्यवस्था में यह भी कह रही है कि अगर कोई आम परिवार एक बच्चे की नीति अपनाकर नसबंदी करा लेंगे तो उन्हें एक बेटा होने के बाद एकमुश्त 80 हजार रुपये, और एक बेटी के बाद नसबंदी होने पर सीधे एक लाख रुपये की आर्थिक मदद होगी। असम का मामला भी कुछ इसी तरह का है वहां जनसंख्या बढ़ोतरी बहुत तेजी से तो नहीं हो रही है लेकिन राज्य के भाजपा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का कहना है कि राज्य के कुछ हिस्सों में जनसंख्या विस्फोट है और यह राज्य के विकास में बाधा हो सकता है।
अब अगर हम भाजपा की साख को 2 मिनट के लिए अलग रखें कि उसके बहुत सारे कार्यक्रम मुसलमानों को निशाने पर रखकर बनाए जाते हैं या हिंदुओं को फायदा देने के लिए बनाए जाते हैं, तो हमें इस बात को देखना होगा कि बढ़ती हुई आबादी से किसका फायदा हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश और असम के, या देश में सबसे अधिक तेज रफ्तार से आबादी बढ़ाने वाले बिहार के मुस्लिम समुदाय में अधिक बच्चे होने से कोई फायदा हो रहा है? मुस्लिमों के बीच पढ़ाई-लिखाई कम है, उनके अधिकतर लोग मिस्त्री-मैकेनिक जैसे छोटे काम में ही सीमित रह जाते हैं, ड्राइवर-कंडक्टर जैसे कम हुनर वाले काम तक उनकी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। मुस्लिम आबादी का कम अनुपात ही उच्च शिक्षा पाकर बेहतर रोजगार तक पहुंच पाता है। और यह बात महज मुस्लिमों तक सीमित नहीं है दूसरे लोगों पर भी लागू है कि अधिक बच्चे होने से उन्हें आज बेहतर शिक्षा देना नामुमकिन सा हो गया है. किसी भी पार्टी के राज वाले प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पाई गई शिक्षा बच्चों को उच्च शिक्षा के बड़े मुकाबलों के लायक तैयार नहीं कर पाती हैं और महंगी निजी स्कूलों के बाद महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट से होकर ही बच्चे इन बड़े मुकाबलों के लायक अपने आपको पाते हैं। इस बात के खिलाफ कई किस्म के अपवाद गिनाए जा सकते हैं लेकिन हम अभी व्यापक आंकड़ों से निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर यह कह सकते हैं कि किसी भी जात और धर्म के परिवारों में जितने अधिक बच्चे होते हैं उनके अच्छे पढ़ने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है, उनके अच्छे खाने पीने की संभावना भी उतनी ही कम हो जाती है, उनके अच्छे रहन-सहन की संभावना भी उतनी ही कम हो जाती है। इसलिए परिवार में बच्चों की गिनती कम होना हर जाति और धर्म के लिए एक बेहतर नौबत है।
सवाल यह है कि अगर मुस्लिम समाज में अधिक बच्चों की अभी तक चली आ रही प्रथा पर असम या उत्तर प्रदेश के इन नए नियमों से कोई नया वार होने जा रहा है? यह समझने की जरूरत है कि यह वार है, या इन समुदायों के लिए फायदे की बात है? हम इन समुदायों को, खासकर मुस्लिम समुदाय को जब देखते हैं, तो यह साफ दिखाई पड़ता है कि एक मुस्लिम महिला की अपनी इच्छा की बहुत अधिक जगह मुस्लिम सामाजिक व्यवस्था के भीतर नहीं है, और एक मुस्लिम महिला से कितने बच्चे पैदा हों, इन्हें आमतौर पर उसके शौहर को ही तय करने दिया जाता है। ऐसे में यह नई व्यवस्था अगर मुस्लिम समाज के कुछ लोगों को कम बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित या मजबूर करती है, तो इससे कम से कम उतने परिवारों में मुस्लिम महिला की स्थिति भी बेहतर होगी, जो आज ना केवल अधिक बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर है बल्कि अधिक बच्चों की देखभाल करने के लिए, उन्हें बड़े करने के लिए, और फिर उन बच्चों की बाकी जिंदगी फिक्र करने के लिए भी मजबूर हैं। आज चाहे मुस्लिम समाज में अधिक बच्चों को पैदा करने की आजादी इस नए कानून के तहत कुछ सीमित होने जा रही है, तो भी यह सोचने की जरूरत है कि यह सीमा किसके लिए नुकसानदेह है और किसके लिए फायदेमंद है?
अगर एक मुस्लिम का परिवार छोटा होगा तो उससे उसी का फायदा है, उसके बचे हुए पैसों से हिंदू समाज का कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। अगर मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति को अधिक बच्चे पैदा करने में दिलचस्पी है, तो उसे पंच-सरपंच का चुनाव लड़ने नहीं मिलेगा, उसे वार्ड या महापौर का चुनाव लड़ने नहीं मिलेगा, उसे सरकारी नौकरी के लिए अर्जी देने नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बच्चे पैदा करने पर कोई रोक नहीं है। उसे सीमित बच्चों के लिए लिए रियायती राशन मिलेगा लेकिन यह संख्या हिंदू परिवार के लिए भी लागू होगी जहां पर दो से अधिक बच्चे होने पर कोई हिंदू भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा या किसी हिंदू परिवार को भी रियायत राशन 2 बच्चों से अधिक के लिए नहीं मिल सकेगा। आज ऐसे हिंदू परिवार भी कम नहीं हैं, जहां पर बेटे की चाह में चार-चार, पांच-पांच बेटियां हो जाती हैं और उसके बाद बुढ़ापे में जाकर एक बेटा नसीब हो पाता है। ऐसे हिंदू परिवार भी चुनाव लड़ने या रियायती राशन पाने के हक से वंचित रह जाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश और असम के यह कानून जिन लोगों को मुस्लिम समाज को चोट पहुंचाने वाले लग रहे हैं उन्हें लगते रहे, हम तो इन्हें मुस्लिम समाज के फायदे के कानून मान रहे हैं कि परिवार का आकार सीमित रखकर वे अपने कम बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, बेहतर खानपान दे सकते हैं, उनका इलाज करा सकते हैं और एक मुस्लिम महिला की हालत भी उससे बेहतर ही हो सकती है।
छत्तीसगढ़ जैसे राज्य ने भी पिछली भाजपा सरकार के दौरान यह व्यवस्था देखी हुई है कि जब पंच-सरपंचों के लिए 2 बच्चों की अनिवार्यता लागू की गई थी, और बहुत से ऐसे मामले हुए थे जिनमें तीसरा बच्चा पैदा होने के बाद पंच सरपंच की पात्रता खत्म कर दी जाती थी, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता था. बाद में भाजपा सरकार के चलते हुए ही विरोध की वजह से इस व्यवस्था को बदला गया था। हमने उस वक्त भी लगातार इस बात को लिखा था कि यह व्यवस्था कई मायनों में नाजायज है। इसलिए नाजायज थी कि इसे लागू करने वाले विधायकों ने इसे अपने ऊपर लागू नहीं किया था। इसे सिर्फ गांव के पंच-सरपंच पर लागू किया गया था मानो गांव में पढ़ने वाली आबादी सांसदों और विधायकों के रास्ते बढ़ने वाली आबादी से अधिक खतरनाक होती है।
खैर यह व्यवस्था खत्म हुई और आज उत्तर प्रदेश और असम में इसे लागू करने पर चर्चा हो रही है तो हम इस बात को साफ लिखना चाहते हैं कि यह व्यवस्था आज के बाद पैदा होने वाले बच्चों के परिवारों पर ही लागू होनी चाहिए, और अगर पहले से किन्हीं लोगों के दो से अधिक बच्चे हैं, तो उन पर यह व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह व्यवस्था स्थानीय संस्थाओं के बजाय देश के हर किस्म के चुनाव पर लागू होनी चाहिए और 9 बच्चों के मां-बाप सांसद या विधायक क्यों बन सकें अगर उन्हें पंच सरपंच बनने के लिए अपात्र माना जा रहा है, या जैसा कि उत्तर प्रदेश में शहरी निकायों में भी चुनाव के लायक नहीं माना जा जा रहा है। हमारा मानना है कि ऐसी असमान व्यवस्था असंवैधानिक होगी और इसे संसद और विधानसभा तक लागू करना ही होगा। सांसद और विधायक को अधिक बच्चे पैदा करने का सुख या मनमर्जी देने का कोई लोकतांत्रिक कारण नहीं हो सकता, और यह व्यवस्था सभी के लिए खत्म होनी चाहिए।
हम खुद मुस्लिम समाज के हित के लिए यह बात चाहते हैं कि अगर वे अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उन्हें अपने परिवार के आकार को सीमित रखने के लिए यह एक अच्छी वजह मिल रही है कि वह सरकारी नौकरी के हकदार बनने के लिए या किसी चुनाव को लड़ने के लिए अपने परिवार के आकार को सीमित रखें। जिन लोगों को किसी सरकारी रियायत की फिक्र नहीं है और जिन्हें अपने कितने भी बच्चों को पढ़ाने और उनका इलाज कराने की ताकत हासिल है, वह लोग जरूर जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, और उसके बाद उन्हें कोई शिकायत भी नहीं होनी चाहिए। चुनाव की पात्रता पंचायत से लेकर संसद तक तक तक सब जगह लागू हो, और जनकल्याण की कुछ गरीब केंद्रित योजनाओं के लिए बच्चों की संख्या को कोई सीमा न बनाया जाए। बाकी इस कानून में हमको कोई बुराई नहीं दिख रही है और यह कानून लागू किया जाना चाहिए। जिन लोगों को यह लगता है कि यह कानून मुस्लिम समाज पर एक हमला है और वह मुस्लिमों के हितैषी होने के नाते उनके हक के लिए इस कानून का विरोध करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए हमारा यह मानना है कि यह लोग मुस्लिम समाज के विरोधी हैं और यह मुस्लिम समाज के नुकसान का ही काम कर रहे हैं अगर यह उसके लोगों को बच्चों की संख्या सीमित रखना नहीं समझा पा रहे हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)