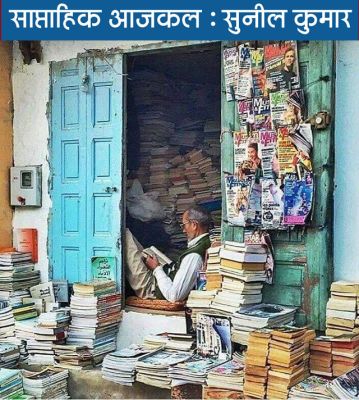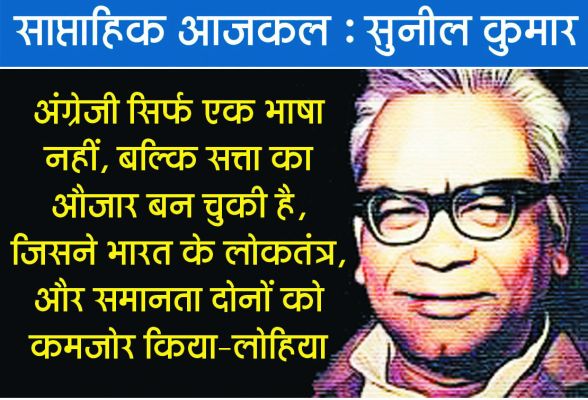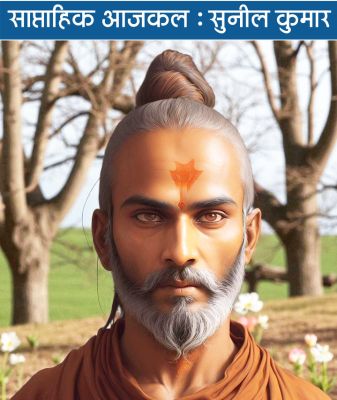आजकल

कभी-कभी मेरे सामने यह धर्मसंकट रहता है कि इतवार को एक ही वक्त पर, एक के बाद एक लिखे जाने वाले, संपादकीय, और इस साप्ताहिक स्तंभ ‘आजकल’ के विषय क्या हों? कभी-कभी यह भी होता है कि इनमें से किसी एक को लिखना शुरू करता हूं, और वह बगल की जगह के लायक अधिक बनने लगता है, तो फिर उस विषय का इस्तेमाल संपादकीय की जगह ‘आजकल’ में हो जाता है, या ‘आजकल’ की जगह संपादकीय में। लेकिन आज इस कॉलम में लिखने के लिए जो मुद्दा है, वह इसी के लायक है, और संपादकीय खत्म करने के बाद अब जब इस पर लिखना शुरू कर रहा हूं, तो तस्वीर बिल्कुल साफ है कि इसे अखबार की सोच की तरह लिखना जायज नहीं हो सकता, मेरी निजी सोच की तरह लिखना ही सही होगा।
भारत एक मामले में एक जीवंत लोकतंत्र है कि यहां अलग-अलग विचारधाराओं से लिखा जाना, कम से कम अब तक तो, जारी है। सहमति और असहमति का अनुपात कम-अधिक हो सकता है, लेकिन असहमति पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई है। सत्ता पर असहमति को कुचलने की तोहमतें बहुत लगती हैं, बहुत से मामलों में ऐसा लगता है कि असहमत लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है, फिर भी मेरे सीने में नहीं तो, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन, आग जलनी चाहिए। हिन्दुस्तान में आग इतनी तो जल ही रही है कि आग अभी बाकी है। पंजाब की बस्तियों में कहा जाता है कि चूल्हा सुलगाने के लिए पड़ोस से आग ले आओ, ठीक उसी तरह जैसे कि दही जमाने के लिए पड़ोस से जामन ले आओ। ऐसे ही असहमति की आग भी इस देश के मीडिया में, सोशल मीडिया में, राजनीतिक दलों में, राज्यों में, कहीं न कहीं, हर कहीं जलती-सुलगती रहती ही है। कोई भी सरकारी दमकल इतनी ताकतवर नहीं हो पाई है कि वह हर सुलगती आँच को बुझा दे।
अब ऐसे में कई लोगों को मुझसे यह शिकायत रहती है कि मैं किसी व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ, किसी विचारधारा या किसी धर्म-संप्रदाय के खिलाफ ‘उतना’ हमलावर होकर नहीं लिखता, और यूट्यूब पर उतना आक्रामक नहीं रहता, जितने कि कुछ और लोग रहते हैं। और यह शिकायत किसी एक विचारधारा की नहीं रहती, अलग-अलग मौकों पर अलग-अलग कई विचारधाराओं को यही शिकायत रहती है कि आप करीब रहकर भी उतने करीब नहीं हैं जितने कि फलां-फलां हैं।
लोगों की यह शिकायत एकदम सही इसलिए रहती है कि किसी के करीब रहना पहली बात तो यह कि मेरा मकसद नहीं है, दूसरी बात यह कि मेरे पेशे की ऐसी जरूरत भी नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति, पार्टी, या विचारधारा के करीब रहूं, या उसके खिलाफ रहूं। मेरी विचारधारा अखबारनवीसी से परे की कुछ नहीं है, और अखबारनवीसी किसी एक विचारधारा पर नहीं चलती, वह मूल्यों पर चलती है। मैं कम से कम अपने लिखने और बोलने में विचारधारा, और मूल्यों में फर्क करके चलता हूं। विचारधारा तो अलग-अलग राजनीतिक दलों की अलग-अलग हो सकती है, और किसी समय किसी एक मुद्दे पर लिखते हुए हो सकता है कि वह लिखना किसी एक दल को ज्यादा माकूल बैठे, और किसी दूसरे वक्त किसी दूसरी पार्टी को। लेकिन पत्रकारिता, और लोकतंत्र के जो बुनियादी मूल्य हैं, वे तो पार्टियों की सरहदों से परे रहते हैं, और किसी समय वे किसी पार्टी को पसंद हो सकते हैं, किसी और वक्त किसी दूसरी पार्टी को नापसंद हो सकते हैं। सच, लोकतंत्र, और इंसाफ के बुनियादी मूल्यों पर अखबारनवीसी टिकी है, कम से कम मैं इनके बिना अखबारनवीसी की कल्पना नहीं करता।
यह एक अलग बात है कि अखबारनवीसी आज के वक्त में ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह चलन से बाहर हो चुका शब्द बन गई है, और इसकी जगह अभी करीब चौथाई सदी में चलन में बढ़ा शब्द मीडिया इस्तेमाल होने लगा है। मैं अपनी पुरानी दकियानूसी सोच के चलते लुग्दी वाले सस्ते अखबारी कागज पर चलती अखबारनवीसी का हिमायती हूं, और बार-बार इस बात को लिखता भी हूं कि अखबारों को इस आधुनिक, मीडिया नाम की, छतरी से बाहर आना चाहिए, और अपने आपको अपने सदियों पुराने नाम, प्रेस से ही बुलाना चाहिए। प्रेस, और उस पर छपे अखबार मुझे जिन मूल्यों से बांधकर रखते हैं, वे मूल्य आज की डिजिटल-एज में धुंधले हो चले हैं। और भारतीय समाचार चैनलों के साथ अगर कुछ अखबार वाले अपने आपको मीडिया नाम की छतरी के नीचे रखना ठीक समझते हैं, तो उनकी वैसी समझ के साथ मैं किसी बहस में भी शामिल होना नहीं चाहता।
लेकिन इस डिजिटल-एज के योद्धाओं के साथ मेरी तरह के डायनासॉर युग के अखबारनवीस की तुलना ठीक नहीं है। मैं जर्नलिस्ट को कैम्पेनिस्ट (अभियानवादी), और प्रोपेगैंडिस्ट (ढिंढोरची) से परे की एक अलग नस्ल मानता हूं, फिर चाहे वह ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह आज किसी इस्तेमाल और फायदे की न रह गई हो। किसी नेता, पार्टी, या पार्टी की विचारधारा, धर्म, या सम्प्रदाय की सोच के पक्ष या विपक्ष में मुहिम चलाने वालों, उनका जिंदाबाद-मुर्दाबाद किस्म का जर्नलिज्म करने वालों से अपनी कोई तुलना मुझे नाजायज ही लगती है। बहुत से लोग हैं जिनका काम एक एजेंडा के तहत है, उसका हिस्सा ही है। लेकिन मैंने अपने लिए अपने काम की सीमा को सच, लोकतंत्र, और इंसाफ तक सीमित रखा हुआ है। इन जेनेरिक दवाओं के बाद मुझे अलग-अलग ब्राँड की दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती। और दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों को जेनेरिक से कैसी चिढ़ रहती है, यह तो सबको मालूम ही है। लोगों को यह भी मालूम है कि ब्राँड दवाओं के कारोबार की कमाई कितनी और कैसी रहती है। कुछ वैसा ही हाल आज के वक्त अच्छे-बुरे कैसे भी अखबारों को छोडक़र बाकी किस्म के मीडिया का है, और वह ब्राँड प्रमोशन में लगा हुआ है।
यह देखकर भी थोड़ी सी हैरानी होती है कि प्रेस से परे का ऐसा मीडिया किस तरह स्टेडियम की सीमा रेखा से परे दर्शकों को गुदगुदाने के लिए चीयरलीडर्स की तरह काम करके फख्र हासिल करता है। इस काम में भी अखबारनवीसी अभी मोटेतौर पर दाखिल नहीं हो पाई है, और पल्प-फिक्शन अभी सिर्फ उपन्यासों तक सीमित शब्द है, लुग्दी-कागज पर छपने वाले अखबारों के लिए अभी भी पल्प-फिक्शन जैसी गाली नहीं दी जा रही।
एक बार फिर उन बातों पर लौटूं जिनकी वजह से आज इस पर लिखना सूझा, तो अखबारनवीसी, और बाद में आए दूसरे किस्म के मीडिया नाम के तरह-तरह के धंधों के लिए मेरी नजर में मूल्यों पर बने रहना ही सबकुछ है, उनका भाड़े के भोंपुओं की तरह काम करना कम से कम प्रेस के दायरे में तो नहीं आता है। चूंकि भोंपू इतने बड़े-बड़े हैं कि अखबारों की लुग्दी बनाकर भी उनका मुंह बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए अखबारों को ऐसे शोरगुल से बाहर आ जाना चाहिए, मीडिया नाम की छतरी छोडक़र अपने माथे पर प्रेस का स्टिकर लगाकर चलना चाहिए, और इज्जत की जिंदगी जीना चाहिए, इज्जतदार काम करना चाहिए। अखबारनवीसों को कभी भी मिलते-जुलते धंधों में नामी-गिरामी हो चुके पांच सितारा दिग्गजों से न तो रश्क करना चाहिए, और न ही उनकी बराबरी की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मुझको जब लोग कैम्पेनिस्ट और प्रोपेगेंडिस्ट न पाकर कुछ निराश होते हैं, तो मेरे पास उन्हें देने के लिए किसी सफाई की जरूरत नहीं रहती। मैं उनकी तकनीक ईजाद होने के पहले से अखबारनवीस रहा हूं, और मेरे लिए किसी नेता, या पार्टी की साख बनाने या बिगाडऩे की सुपारी उठाना जरूरी नहीं रहता। महाराष्ट्र में पैदा होने की वजह से बचपन से मैं सुपारी को चबाना ही जानता हूं, उठाना आज तक नहीं सीखा है। मेरा अभी भी मानना है कि अपनी साख खत्म कर देने वाले तथाकथित मीडियाकर्मी उन लोगों का भी भला नहीं करते, जिनका भला करने, और जिनके दुश्मनों का बुरा करने की सुपारी उन्होंने उठाई हुई है। सच के बारे में मैं कई बार लिखता हूं कि वह रेगिस्तान में कहीं-कहीं बिल्कुल अकेले खड़े कैक्टस की तरह कंटीला रहता है, और अकेला भी, उसे सूखी रेत के समंदर के बीच प्यासे जिंदा रहने की आदत भी हो जाती है। इसलिए शोहरत की लहरों पर सवारी कैक्टस के लिए जरूरी नहीं रहती। मैं कुछ उसी किस्म का हूं, और सभी को बराबरी से चुभता भी हूं।