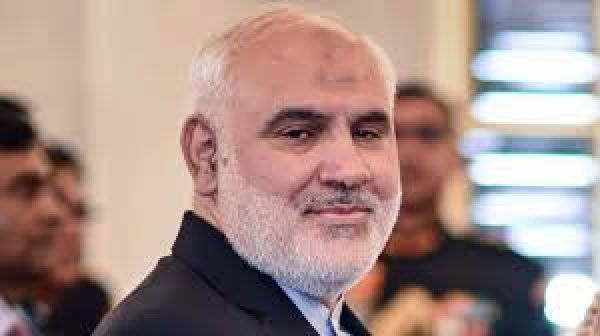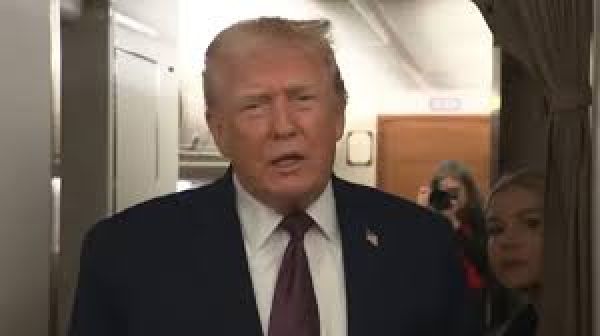अंतरराष्ट्रीय
.jpg)
फ़र्नांडा पॉल
सात अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले और इसके बाद ग़ज़ा पट्टी में इसराइली बमबारी से मौत और तबाही की कई कहानियां बाहर आ रही हैं. पूरी दुनिया में इस इलाक़े में शांति के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं और मार्च निकाले जा रहे हैं.
फ़लस्तीनी लोगों के पक्ष में निकाले जाने वाले इन मार्चों में पारम्परिक कफ़िया पहने प्रदर्शनकारी आम तौर पर दिखते हैं.
कुछ इसे अपने गले में पहनते हैं, कुछ अपने सिर पर. ये इतना अलग दिखता है कि इसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल होता है. एक साधारण सूती गमछा होने से इसका महत्व कहीं अधिक है.
अधिकांश फ़लस्तीनी लोगों के लिए यह संघर्ष और प्रतिरोध का प्रतीक है. एक राजनीतिक और सांस्कृतिक हथियार जो पिछले 100 सालों में प्रासंगिक होता गया है.
यहां तक कि इसे फ़लस्तीन का “अनौपचारिक झंडा” भी कहा जाता रहा है.
इस पहनावे की शुरुआत कहां से होती है? यह कब प्रतीक बना और आज यह कितना अहम है? आज हम इस पर बात करेंगे.
कफ़िया की शुरुआत
हालांकि इसकी सटीक शुरुआत अनिश्चित है, लेकिन कई इतिहासकारों का कहना है कि इसका चलन 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ. ख़ासकर, इराक़ी शहर कुफ़ा में, जिसके नाम पर ही इसे कफ़िया कहा जाने लगा.
कुछ का कहना है कि इसकी शुरुआत इससे भी पुरानी है, शायद इस्लाम से भी पहले.
तथ्य ये है कि साल दर साल इसका इस्तेमाल बढ़ा है. लेकिन इसके पीछे सांस्कृतिक या राजनीतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक कारणों से.
20वीं सदी की शुरुआत में कफ़िया को मुख्य रूप से किसान और घुमंतू अरब खुद को धूप, हवा, रेत या ठंड से बचाव के लिए पहनते थे.
हालांकि शहरों में, फ़लस्तीनियों को इसे पहने देखना आम बात नहीं थी.
वे और महीन कपड़े पहनना पसंद करते थे जैसे फ़ेज़ (जिसे तारबुश भी कहा जाता था). यह एक लाल टोपी होती थी, जिसे ऑटोमन शासक महमूद द्वितीय ने लोकप्रिय बनाया था.
लेकिन कई शोधों से पता चलता है कि 1930 के दशक में फ़लस्तीनी समाज में कफ़िया का एक विशिष्ट अर्थ आकार लेने लगा था. इसके साथ ही इसका इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा.
1936 का विद्रोह
1930 के दशक में फ़लस्तीनी इलाक़े ब्रिटिश शासन के अधीन थे. प्रथम विश्वयुद्ध के बाद लीग ऑफ़ नेशन्स ने इसे यूनाइटेड किंगडम को दे दिया था.
यह शासन 1920 से 1948 के बीच रहा, जिसने फ़लस्तीनियों में असंतोष पैदा किया क्योंकि वे मानते थे कि ब्रिटिश ज़यनिस्ट परियोजना (यहूदी राष्ट्र बनाने के लिए चलाया जाने वाला राजनीतिक अभियान) का समर्थन कर रहे थे.
इसी दौरान यूरोप में जब यहूदी लोगों के ख़िलाफ़ अत्याचार बढ़ गया तो पश्चिम एशिया में यहूदी आबादी का आना भी बढ़ गया.
इस तरह इस इलाक़े में राष्ट्रवादी अरबों की ओर से विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसे “महान अरब विद्रोह” के नाम से जाना जाता है. यह तीन साल 1936 से 1939 तक चला और इस दौरान इस इलाके में काफ़ी टकराव हुए.
इस संघर्ष में कफ़िया ने काफ़ी अहम भूमिका अदा की.
कफ़िया के राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व पर शोध करने वाली इतिहासकार जेन टायनन के अनुसार, “ब्रिटिश की मौजूदगी से फ़लस्तीनी काफ़ी हताश थे और प्रतिरोध करने सबसे अच्छा तरीका था कि पहचान ज़ाहिर न हो...और इस तरह कफ़िया, ब्रिटिश प्रशासन को अचंभे में डालने की रणनीति का हिस्सा बन गया.”
1938 में विद्रोही नेताओं ने शहरों में रहने वाले सभी अरबों से कहा कि वे कफ़िया पहनें.
नीदरलैंड्स की एम्सटर्डम यूनिवर्सिटी से जुड़े शोधकर्ता के मुताबिक, इससे लोगों को पहचानना मुश्किल हो गया और विद्रोहियों को अपनी गतिविधि में आसानी होने लगी...ब्रिटिश सैनिक बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाते थे.
कहा जाता है कि ब्रिटिश इतने परेशान हो गए कि उन्होंने इसे बैन करने की असफल कोशिश भी की.
अ सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ़ कफ़िया के लेखक अनु लिंगाला के अनुसार, यह एक प्रभावी सैन्य रणनीति थी, लेकिन एकजुट प्रतिरोध का प्रदर्शन करने का यह प्रतीक भी बन गया.
उनके अनुसार, “इस परिधान के साथ 1938 में घटी इस घटना को फ़लस्तीनी संस्कृति में अहम मोड़ माना जाता है, जब राष्ट्रवादी मकसद के साथ एकजुटता के पक्ष में और उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ सारे मतभेदों को दरकिनार कर दिया गया.”
जेन टायनन के मुताबिक, उस समय से ही कफ़िया फ़लस्तीनी आत्मनिर्णय, इंसाफ़ और एकजुटता का स्पष्ट प्रतीक बन गया.
“यह विद्रोहियों को ये बताने का तरीक़ा था कि हम सब आपके साथ हैं. ”
कफ़िया क्या है?
वैसे तो कफ़िया अलग अलग रंगों और डिज़ाइन का होता है. लेकिन फ़लस्तीनी लोगों की पहचान बन चुका कफ़िया काला और सफ़ेद होता है और इसके तीन पैटर्न होते हैं.
•जैतून की पत्तियांः यह इलाक़े के जैतून के पेड़ों और इस क़स्बे का इसकी ज़मीन से जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करता है.
• लालः यह फ़लस्तीनी मछुआरों और भूमध्य सागर के साथ उनके संबंध का प्रतिनिधित्व करता है.
•काली रेखाएंः यह फ़लस्तीन के पड़ोसी साझेदारों के साथ व्यापार के रास्ते का प्रतिनिधित्व करता है.
अंतरराष्ट्रीय रूप से यह कैसे लोकप्रिय हुआ?
विद्रोह के बाद के सालों में फ़लस्तीनियों के बीच कफ़िया पहनने का चलन, पहचान के प्रतीक के रूप में फैलना जारी रहा.
इतिहासकार इससे सहमत हैं कि ‘नकबा’ या ‘समूल सफ़ाया’ के बाद इसके चलन में और तेज़ी आई, जब संघर्ष के कारण लाखों फ़लस्तीनी अपने घरों से दर बदर हो गए और इसके बाद 14 मई 1948 को इसराइल का गठन हुआ.
फ़लस्तीनी इतिहास में ‘नकबा’ को सबसे दुखद तारीख़ माना जाता है.
लेकिन 1960 के दशक तक कफ़िया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय नहीं हुआ था.
फ़लस्तीनी हितों का चेहरा बन चुके यासर अराफ़ात के कारण कफ़िया व्यापक रूप से लोकप्रिय हुआ.
बिना कफ़िया के अराफ़ात की शायद ही कोई तस्वीर मिले. सीरिया, जॉर्डन और लेबनान में लड़ाई के दौरान उन्होंने इसे ही पहन रखा था. जब 1974 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में फ़लस्तीनियों के पक्ष में भाषण दिया तो 20 साल बाद जब उन्होंने ओस्लो में नोबेल शांति पुरस्कार ग्रहण किया.
जेन टायनान के अनुसार, “राजनीतिक बयान देते समय वो आम तौर पर कफ़िया ही पहनते थे. वो अपने दाहिने कंधे पर इस तरह त्रिभुजाकार रखते थे कि यह 1948 के पहले वाले फ़लस्तीन का आकार लगे.”
अनु लिंगाला के अनुसार, बाद में जब इसराइल ने फ़लस्तीनी झंडे को प्रतिबंधित कर दिया (1967 में हुए छह दिन के युद्ध के तुरंत बाद और 1993 में ओस्लो संधि से पहले तक), कफ़िया और बड़ा प्रतीक बनकर उभरा.
शोधकर्ताओं का कहना है कि विनाशकारी छह दिन के युद्ध के बाद ही राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसका महत्व बढ़ा.
बाद के सालों में फ़लस्तीनी क्षेत्र की सामूहिक पहचान और उनकी ज़मीन के अधिकार पर जैसे जैसे ख़तरा बढ़ा, एकता और पहचान के सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में कफ़िया का महत्व भी बढ़ता गया.
यहां तक कि इसे महिलाएं भी इस्तेमाल करने लगीं.
प़ॉपुलर फ़्रंट फ़ॉर द लिबरेशन ऑफ़ पैलेस्टाइन की सदस्य लीला ख़ालेद की एके-47 राइफ़ल के साथ कफ़िया पहने एक तस्वीर 1969 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चित हुई.
अंग्रेज़ी अख़बार द गार्डियन को बाद में ख़ालिद ने बताया कि एक महिला के तौर पर उन्हें ये दिखाना था कि हथियारबंद संघर्ष में वे भी आदमियों के बराबर हैं, “यही कारण है कि हम मर्दों की तरह होना चाहते थे, दिखने में भी.”
“फ़ैशनेबल” पहनावा
जेन टायनन के अनुसार, उपरोक्त कारणों से कफ़िया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धीरे-धीरे एक फ़ैशनेबल पहनावा बन गया, ख़ासकर पश्चिम में.
उनके मुताबिक, “उत्तरी अमेरिका और यूरोप में मीडिया में आने की वजह से कफ़िया लोकप्रिय हुआ और फिर यह बहुत आकर्षक और फ़ैशन बन गया.”
उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि 1970 के दशक तक पश्चिम में नौजवान “प्रभावी पूंजीवादी संस्कृति और उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ प्रतिरोध” के तौर पर सैन्य स्टाइल वाले कपड़े पहनते थे.
टायनान के अनुसार, इससे पता चलता है कि पश्चिमी एशिया के बाहर कफ़िया कैसे इतना लोकप्रिय हुआ.
1990 के दशक में दुनिया की कुछ बड़ी शख़्सियतें भी इसे पहनने लगीं. इन्हीं में से थे अंग्रेज फ़ुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम और संगीतकार रोजर वाटर्स भी शामिल थे.
बाद में अमेरिकी ब्रांड अरबन आउटफ़िटर्स ने नामचीन फ़ैशन स्टोर में इसे बेचना शुरू किया और गिवेंची या लुई विट्टॉन जैसे डिज़ाइल कलेक्शन भी कफ़िया को इस्तेमाल करने लगे.
इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि इसका अधिकांश प्रोडक्शन चीन चला गया.
आज सिर्फ़ एक फ़लस्तीनी फ़ैक्ट्री बची हुई है जिसे यासर हिरबावी ने 1961 में स्थापित किया था, जो वेस्ट बैंक के हेब्रान सिटी में है.
प्रतिरोध की ताक़त
हालांकि कुछ हद तक कफ़िया फ़ैशनेबल चीज़ बन चुकी है, इतिहासकार मानते हैं कि बावजूद इसके इसका राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व कभी कम नहीं हुआ.
आज जब ग़ज़ा पट्टी में युद्ध चल रहा है, कफ़िया ने नई प्रासंगिकता ग्रहण कर ली है.
यहां तक कि इस पर विवाद भी हुआ और दुनिया के कुछ देश इसके पहनने पर पाबंदी भी लगा चुके हैं, जैसे- जर्मनी.
अनु लिंगाला के अनुसार, “आज कफ़िया की ताक़त फ़लस्तीनी प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में अभी भी बरकरार है. फ़लस्तीनी समर्थक शांत तरीके से लेकिन इस मुद्दे के प्रति दिल से एकजुटता दिखाने के लिए इसे पहनते हैं.”
जेन टायनन के अनुसार, “यह बहुत दिलचस्प है कि पूरी दुनिया में कपड़े के इस टुकड़े को लेकर लोगों की गजब की समझदारी है. यह बहुत असाधारण है, लगभग अभूतपूर्व.” (bbc.com)