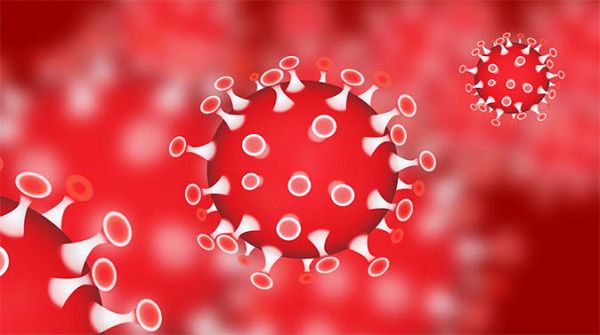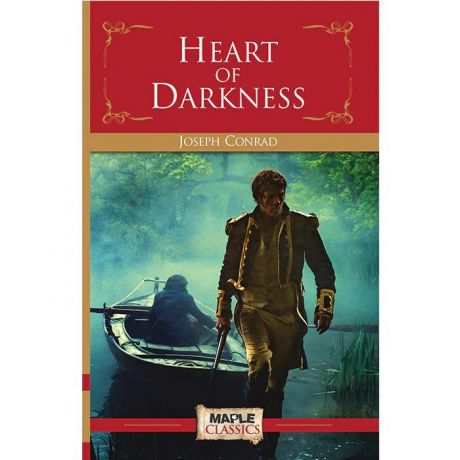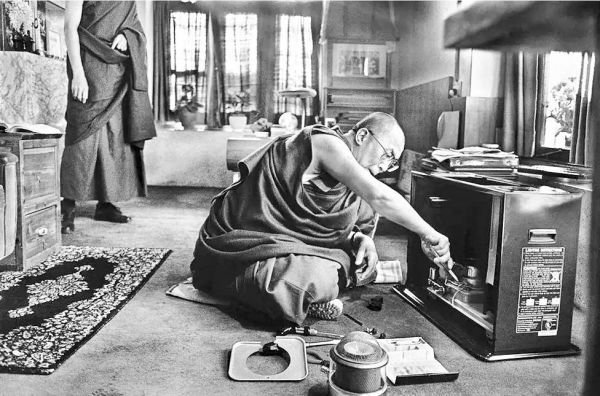विचार/लेख
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
पाकिस्तान के शहर पेशावर में हुए विस्फोट ने पूरे देश और सरकार को हिलाकर रख दिया है। शाहबाज़ सरकार आर्थिक संकट से पहले ही जूझ रही है, अब इस विस्फोट ने जले पर नमक छिड़क दिया है। इस विस्फोट में हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग 100 लोग तो मर चुके हैं और डेढ़ सौ लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। यह विस्फोट भी कहां हुआ है? पेशावर की एक मस्जिद में। और वह किस वक्त हुआ है? दोपहर की नमाज के वक्त! दूसरे शब्दों में तहरीके-तालिबान के आतंकवादियों ने इस्लाम का भी अपमान कर दिया है। वे लोग अपने को कट्टर इस्लामी कहते हैं और उन्होंने मस्जिद में ही विस्फोट करवा दिया। इस्लामी राष्ट्र होने का दावा करनेवाला पाकिस्तान इस घटना से कोई सबक सीखेगा या नहीं? उसने आतंकवाद को इसलिए बढ़ावा दिया कि वह भारत से कश्मीर छीन सकेगा।
उसने भारत से लड़े युद्धों में विफल होने के बाद आतंकवाद को ही अपना हथियार बनाया लेकिन अब मियां की यह जूती मियां के सिर ही पड़ रही है। दहशतगर्दी के चलते जितने लोग भारत में मरते रहे हैं, उनसे कहीं ज्यादा पाकिस्तान में मर रहे हैं। पिछले साल एक शिया मस्जिद पर हुए हमले में दर्जनों लोग मारे गए थे। इसी पेशावर में 2016 में हुए हमले के कारण लगभग डेढ़ सौ मासूम बच्चे कुर्बान कर दिए गए थे। वे बच्चे एक फौजी स्कूल में पढ़ रहे थे। इस मस्जिद में अभी मृतकों में ज्यादातर पुलिस के अफसर और जवान ही हैं। इस हमले की जिम्मेदारी ‘तहरीके-तालिबान पाकिस्तान’ के कमांडर ने ली है। उसने कहा है कि यह हमला उस हत्या का बदला हे, जो पिछले साल अगस्त में टीटीपी के कमांडर उमर खालिद खुरासानी की काबुल में की गई थी। ‘तहरीक’ यों तो पाकिस्तानियों का संगठन है लेकिन यह अफगानिस्तान के तालिबान के साथ गहरे में जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार और पाकिस्तानी सरकार के बीच भी लगातार खटपट चल रही है। ‘तहरीक’ के नेता पठान हैं और तालिबान भी पठान हैं।
दोनों पंजाबी वर्चस्व के खिलाफ कटिबद्ध हैं। इसीलिए डूरेन्ड लाइन पर भी फिर से विवाद छिड़ गया है। कितने आश्चर्य की बात है कि काबुल की तालिबान सरकार को अभी तक पाकिस्तान सरकार ने औपचारिक मान्यता भी नहीं दी है। पाकिस्तान के गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि इस हमले का इस्लाम से कुछ लेना-देना नहीं है। नमाज़ पढ़ते हुए मुसलमानों पर हमला करना कुरान की शिक्षा के विरुद्ध है। यदि यह बात ठीक है तो यह मानना पड़ेगा कि या तो पाकिस्तानी तालिबान मुसलमान नहीं हैं या जो लोग मारे गए हैं, उन्हें तालिबान लोग मुसलमान नहीं मानते। ये दोनों बातें गलत हैं। मरनेवाले और मारनेवाले दोनों ही मुसलमान हैं। इस्लाम का इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहे हैं। (नया इंडिया की अनुमति से)

सुशीला सिंह
क्या आपने कभी ये सवाल सुना है कि एक पुरुष को किस उम्र में पिता बनना चाहिए? शायद ही कभी सुना हो। लेकिन एक महिला को किस उम्र में माँ बनना चाहिए, ये सवाल आपको कभी न कभी, कहीं न कहीं सुनने में जरूर आया होगा।
ये सवाल फिर चर्चा में है और उसका कारण है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का वो बयान, जिसमें उन्होंने महिलाओं के माँ बनने के लिए 22 से 30 साल की उम्र को सही समय बताया है।
गुवाहाटी के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ‘महिलाओं के लिए माँ बनने की सबसे सही उम्र 22 से 30 साल के बीच है। अगर महिलाएँ इसे फ़ॉलो करें, तो माँ और बच्चे दोनों के लिए ये अच्छा होगा।’
सरमा राज्य में जच्चा-बच्चा मृत्यु दर को नीचे लाने की कोशिश से जुड़े एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। वो इस दिशा में अपनी सरकार की कोशिशों की जानकारी दे रहे थे।
उनके मुताबिक़ जल्दी शादी और गर्भाधान जच्चा-बच्चा मृत्यु दर बढऩे की एक अहम वजह है।
उन्होंने कहा, ‘हम लोग नाबालिग़ लडक़ी की ज़बर्दस्ती शादी और उनके जल्दी माँ बनने पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि महिलाओं को शादी करने में बहुत ज्ज्यादा देर भी नहीं करनी चाहिए। ईश्वर ने हमारे शरीर को अलग-अलग उम्र में अलग-अलग चीजें करने के लिए बनाया है।’
सरमा ने ये भी कहा कि 30 के आसपास पहुँच रही महिलाओं को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद से इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि एक महिला को किस उम्र में बच्चा पैदा करना चाहिए?
बहस की शुरुआत
एक पक्ष का कहना है कि एक महिला का अपने शरीर पर अधिकार है और उस पर फ़ैसला लेने का उसे पूरा अधिकार है यानी वो कब माँ बनना चाहती है और कब तक नहीं बनना चाहती है, यह वही तय करेंगी।
महिला मुद्दों पर काम करने वाली कार्यकर्ताओं ने हिमंत बिस्वा सरमा के इस बयान की आलोचना की है और कहा है कि किसी भी व्यक्ति चाहे वो कोई भी पद पर हो, उसे हक नहीं है कि वह ये बताए कि कोई महिला किस उम्र में माँ बने?
हालाँकि कुछ डॉक्टरों के मुताबिक एक महिला के माँ बनने की उचित उम्र 20 से 30 साल के बीच होती है और वो इसके मेडिकल कारण भी बताते हैं।
स्त्री रोग विशेषज्ञ शालिनी अग्रवाल कहती हैं कि एक निश्चित उम्र में अगर महिला माँ बनती है, तो यह उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है क्योंकि एक उम्र के बाद महिला के शरीर में अंडे बनने कम हो जाते हैं।
वे कहती हैं, ‘30 साल की एक महिला में अंडों की संख्या ठीक-ठाक होती है और वो कंसिव कर पाती है, लेकिन 30 की उम्र के बाद महिलाओं में अंडे कम होने लगते हैं और 35 के बाद इनकी संख्या की कमी के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है और इससे पैदा होने वाले बच्चे में किसी विकार उपन्न होने की आशंका बढ़ जाती है।’ऐसे में अगर महिला माँ बनने पर विचार कर रही है, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा 35 की उम्र तक माँ बन जाना चाहिए क्योंकि इसके बाद इन्फर्टिलिटी की दिक्कतें आ सकती हैं। शालिनी अग्रवाल ये भी कहती है कि करियर को अहमियत दी जानी चाहिए, लेकिन मातृत्व और करियर के बीच संतुलन बनाने की ज़रूरत है।
मातृत्व और करियर का द्वंद्व

सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की निदेशक और महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली रंजना कुमारी का कहना है कि इस मामले पर कोई डॉक्टर या विशेषज्ञ एक सुझाव दे सकते हैं, लेकिन किसी राजनीतिज्ञ का इस मुद्दे पर बोलना हास्यास्पद है और इसकी आलोचना होनी चाहिए।
वे कहती हैं, ‘हमने आईटी, बैंकिंग और ट्रैवल टूरिज़्म के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को लेकर शोध किया था। हमने देखा था कि उन महिलाओं को बड़े पद ऑफर किए गए, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका ट्रांसफर हो रहा था या फिर उनके लिए घर और
ऑफिस के बीच सतुंलन बनाना मुश्किल हो रहा था।’
तो सवाल यही उठता है कि क्या महिलाओं के लिए पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियाँ सर्वोपरि हो जाती हैं?
भारत में एक बच्चा पैदा करने करने से लेकर उसके पालन पोषण की जि़म्मेदारी मुख्यत:एक महिला की ही समझी जाती है और समाज में ज्वाइंट पैरेटिंग या जिसमें माँ-पिता दोनों पूरी जिम्मेदारी लें, ऐसी कोई अवधारणा ही नहीं है।
रंजना कुमारी कहती हैं कि आजकल ये देखा जाने लगा है कि कुछ महिलाएँ बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहतीं या देर से शादी करना चाहती हैं, जिसका समाज में आदर किया जाना चाहिए।
वहीं तकनीक ने इतना विकास कर लिया है कि वे बच्चे जब चाहें, तब कर सकती हैं तो ऐसे में वो स्वच्छंद हो कर फैसला क्यों नहीं ले सकतीं?
वहीं जलवायु परिवर्तन, कॉरपोरेट सेक्टर और विकास जैसे मुद्दों को महिलाओं के नज़रिए से भी कवर करने वाली पत्रकार अदिति कपूर कहती हैं कि एक महिला पर बच्चा पैदा करने और करियर बनाने का बोझ एक साथ होता है। ऐसे में उनके लिए ऐसी सुविधाएँ दिए जाने की ज़रूरत है, जो उसे सहयोग कर सकें।
वे कहती हैं, ‘महिलाओं पर बच्चा पैदा करने का बॉयोलॉजिकल दबाव रहता है। पुरुषों के लिए पैटरनिटी लीव का प्रावधान वर्षों बाद आया। हालाँकि सरकारी नौकरी में वो 15 दिन के लिए है, वहीं प्राइवेट में ये कम है या है ही नहीं। ऐसे में महिलाओं के सहयोग के लिए ऐसी सुविधाओं को और मज़बूत बनाना चाहिए और उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। आखिर वो भी तो जीडीपी में योगदान दे रही हैं।’
इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सुचित्रा दलवी कहती हैं, ‘एक माँ चाहे वो संगठित या अंसगठित क्षेत्र में काम करती हो, उसके बच्चे की देखरेख के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए। वहीं औरतों में नौकरी की सुनिश्चितता होनी चाहिए। घर में पुरुष को भी पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए क्योंकि वो केवल माँ का ही बच्चा नहीं है, पैटरनिटी लीव का समय बीतने के बाद भी बच्चे की जिम्मेदारी बनी रहती है।’
सुचित्रा एशिया सेफ अबॉर्शन पार्टनरशिप नाम से काम कर रहे नेटवर्क की संयोजक और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं।
महिलाओं की अर्थव्यवस्था में भागीदारी
भारत में कामकाजी महिलाएँ अपनी प्रतिभा और निष्ठा से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अर्थव्यवस्था में भी अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं।
भारतीय उद्योग परिसंघ या सीआईआई की वेबसाइट पर छपे एक लेख के मुताबिक भारत में 43.2 करोड़ महिलाएँ काम करने की उम्र में हैं, जिनमें से 34.3 करोड़ महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में काम कर रही हैं।
मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने आकलन किया है कि अगर महिलाओं को समान मौक़े दिए जाते हैं, तो साल 2025 के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 77000 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है।
वहीं फिलहाल सकल घरेलू उत्पाद में उनकी भागीदारी 18 फीसदी है।
हालाँकि महिला विशेषज्ञों का कहना है कि अगर असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी जोड़ ली जाएगी, तो जीडीपी में उनकी हिस्सेदारी कहीं अधिक हो जाएगी।
वहीं ग्रामीण स्तर पर भी महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं और पंचायत स्तर पर दिए गए आरक्षण ने उन्हें और सशक्त बनाने में मदद की है।
वहीं स्टार्ट अप के क्षेत्र में भी कई महिलाएँ आगे आई हैं।
समाज में बदलाव
डॉक्टर सुचित्रा दलवी कहती हैं कि समाज में एक महिला के लिए अभी शादी करना और बच्चे पैदा कहना अनिवार्य माना जाता है, बल्कि ये चॉइस होना चाहिए।
उनके अनुसार, ‘हर औरत के पास यूटेरस है तो इसका मतलब ये कतई नहीं समझा जाना चाहिए कि वो माँ ही बनना चाहती है या बनना चाहिए। उसे उसके शरीर और जिंदगी पर अधिकार दिया जाना चाहिए।’
‘हाँ बॉयोलॉजिकली देखें तो सही है क्योंकि 20 से 30 साल की उम्र में एक लडक़ी में फर्टिलिटी भी बढिय़ा रहती है और सेहत भी अच्छी होती है। अगर बीपी या शुगर के खतरे की बात करें, तो 40 की उम्र के बाद यह ज्यादा होता है।’
विशेषज्ञों का कहना है कि ये समाज की विडंबना है कि 21वीं सदी में भी एक महिला को केवल माँ, बेटी, पत्नी के रूप में देखा जाता है, जिन्हें जिम्मेदारियों की बेडिय़ों में जकड़ दिया जाता है, लेकिन उनसे ये नहीं पूछा जाता कि आखिर वो क्या चाहती हैं।
हालाँकि बदलते समय के साथ समाज में पनपती चली आ रही इस सोच को बदलने और महिलाओं की इच्छाओं को अहमियत देने की ज़रूरत है। (bbc.com/hindi)
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी की भारत-जोड़ो यात्रा का आज समापन हो गया है। केरल से कश्मीर तक की यह यात्रा शंकराचार्य के अलावा भारत में अब तक राहुल के सिवाय शायद किसी और ने कभी नहीं की। यह यात्रा इस अर्थ में एतिहासिक है। लेकिन भारत कहां से टूट रहा है, जिसे जोड़ने के लिए राहुल ने यह बीड़ा उठाया है? इस यात्रा का नाम यदि ‘कांग्रेस जोड़ो’ होता तो कहीं बेहतर होता। कांग्रेस टूट ही नहीं रही है, वह दिवंगत होती जा रही है। भारत का विपक्ष अंकुशहीन होता जा रहा है।
राहुल ने श्रीनगर में जाकर कहा कि इस यात्रा ने देश के सामने शासन का वैकल्पिक नक्शा पेश किया है। यदि ऐसा होता तो चमत्कार हो जाता। वह तो बिना यात्रा किए हुए भी पेश किया जा सकता था। यात्रा के दौरान राहुल ने कई ऐसे बयान दे डाले, जो कांग्रेस की ही नीतियों के विरुद्ध थे। जैसे सावरकर की निंदा, जातीय जनगणना का समर्थन, कश्मीर की ज़मीन पर चीन का कब्जा आदि! इसमें मैं राहुल का कोई दोष नहीं मानता हूं।
यह दोष है, राहुल के आस-पास घिरे हुए खुशामदियों का! वे लकड़ी के गुड्डे में जैसी और जितनी चाबी भर देते हैं, वह भोला भंडारी वैसा ही नाच दिखा देता है। राहुल को एक मूल मंत्र किसी ने पकड़ा दिया। वह है- ‘नफरत के बाजार में, मैं मुहब्बत की दुकान खोलने आया हूं।’ सारे देश में मुहब्बत की दुकान खोलने से बेहतर होता कि वह अपने लिए ही मुहब्बत की कोई दुकान खोल लेता। शादी कर लेता। राहुल अपनी बहन प्रियंका वाड्रा से ही कुछ सीख लेता। जो खुद के लिए अब तक मुहब्बत की दुकान नहीं खोल सका, वह देश के लिए मुहब्बत की दुकान कैसे खोलेगा?
राहुल सुंदर है, स्वस्थ है, सदाचारी है। संपन्न और जाने-माने घर का युवक है। वह साधुओं और मौलानाओं का भेस बनाकर क्यों घूम रहा है? क्या वह मोदी की नकल कर रहा है? वह गांधी की नकल करता तो कहीं बेहतर होता! उसे फिरोजगांधी का वंशज नहीं, महात्मा गांधी का उत्तराधिकारी माना जाता! गांधी उपनाम को वह सार्थक कर देता। उसकी दादी इंदिराजी यदि अपने नाम के आगे गांधी उपनाम नहीं लगातीं तो भी उनका नाम काफी बड़ा हो गया था।
इस भारत जोड़ों का लाभ कांग्रेस को कितना मिलेगा, इस पर कांग्रेसी नेताओं को ही बड़ा शक है लेकिन राहुल गांधी को इसका जबर्दस्त लाभ मिल रहा है। देश का हर नेता अपने प्रचार का मोहताज होता है। वे आत्म-प्रचार पर करोड़ों रु. खर्च कर डालते हैं लेकिन राहुल को एक कौड़ी भी खर्च नहीं करनी पड़ रही है। टीवी चैनलों और अखबारों में पिछले साढ़े चार महिने में राहुल और मोदी लगभग बराबर-बराबर दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि साढ़े चार महिने में उसका जनता से सीधा संपर्क हुआ है, जो 45 साल के राजमहलिया संपर्क से ज्यादा कीमती है। (नया इंडिया की अनुमति से)
- दिलनवाज़ पाशा
सात सितंबर को दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को 136 दिन बाद 14 राज्य का सफ़र करते हुए श्रीनगर में समाप्त हो गई.
कांग्रेस पार्टी के अनुसार, राहुल गांधी की इस यात्रा का घोषित उद्देश्य ''भारत को एकजुट करना और साथ मिलकर देश को मज़बूत करना है."
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बार-बार कहा कि वो देश में नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं.
यात्रा के दौरान जगह-जगह भाषण देते हुए और मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और बेरोज़गारी, महंगाई, भारत के सीमा क्षेत्र में चीन के दख़ल का मुद्दा उठाया.
राहुल गांधी ने कई बार मीडया को भी निशाने पर लिया और भारत के बड़े उद्योगपतियों गौतम अदानी और मुकेश अंबानी पर भी निशाना साधा.
रविवार को राहुल गांधी की यात्रा समाप्त हो गई. इस यात्रा से पहले कई सवाल थे- राहुल गांधी हासिल क्या करना चाहते हैं, क्या वो विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे, क्या वो कांग्रेस को पुनर्जीवित कर पाएंगे?
ऐसे ही कई सवालों पर हमने वरिष्ठ पत्रकारों से बात की, पढ़िए उनका नज़रिया-
अपने ऊपर उठ रहे सवालों को ख़ारिज कर गंभीर नेता के रूप में स्थापित हुए राहुल गांधी
विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार
राहुल गांधी ने क़रीब चार हज़ार किलोमीटर की यात्रा की है. बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने टी-शर्ट पहनकर ये यात्रा की है. टी-शर्ट पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है. इस पर चर्चा करना इस यात्रा को नज़रअंदाज़ करने जैसा है. राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा काम किया है. आज़ाद भारत में चंद्रशेखर की पदयात्रा के बाद ये कोई पहली पदयात्रा हुई है.
राहुल गांधी ने इस यात्रा के ज़रिए उन सभी सवालों को ख़ारिज कर दिया है जो उन पर उठते रहे थे. पहले कहा जाता था कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा, फिर कहा गया कि वो ख़ुद अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन वो नहीं बने, इसके बाद कहा गया कि अध्यक्ष के चुनाव को टाल दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं टाला गया. ऐसा कुछ नहीं हुआ और राहुल गांधी ने जो काम करना तय किया था, वो उसमें लगे रहे और उसे पूरा किया.
भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए राहुल गांधी ने एक मज़बूत और गंभीर नेता की छवि बनाई है. बीजेपी और सोशल मीडिया ट्रोल ने राहुल गांधी की अलग छवि बनाई थी. पहले राहुल गांधी का मज़ाक बनाते हुए मीम सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते थे. अब ये मीम कम हो गए हैं और राहुल गांधी के लिए सकारात्मक कंटेंट सोशल मीडिया पर बढ़ गया है.
इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी की बहुत-सी ख़ूबसूरत तस्वीरें भी आईं. कहीं राहुल बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं बुज़ुर्ग महिला का हाथ थाम रहे हैं तो कहीं आम लोगों को गले लगा रहे हैं. इन तस्वीरें से भी राहुल गांधी की एक सकारात्मक छवि बनी है.
इस यात्रा ने राहुल गांधी के व्यक्तित्व को भी गंभीर बनाया है. हिंदू धर्म में यात्राओं का अहम स्थान रहा है. यात्राएं व्यक्तित्व को गंभीर बनाती हैं. राहुल गांधी ने इस यात्रा के ज़रिए हिंदुस्तान को देखा है, ज़ाहिर है उन्होंने देश के हर गंभीर मुद्दे को भी समझा होगा.
अफ़्रीका से लौटने के बाद जब गांधी भारत आए थे तब उन्होंने भी भारत में यात्राएं कीं और देश को समझा. भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को देश को समझने का मौका दिया है.
राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के मज़बूत नेतृत्व के सामने एक ताक़तवर विकल्प के रूप में खड़े होने की कोशिश भी इस यात्रा के ज़रिए की है. यदि राहुल गांधी को बराबर का नेता ना भी कहें तब भी अब वो कतार में तो आ ही गए हैं. अब लोग राहुल गांधी को गंभीरता से ले रहे हैं.
भारत जोड़ो के नारे में राहुल गांधी कितने कामयाब हुए, ये बाद में पता चलेगा. लेकिन इस दौरान राहुल गांधी जिस तरह लगातार प्रधानमंत्री को घेरते रहे उससे उन्हें फ़ायदा हुआ है. सबसे पहले तो वो कांग्रेस के निर्विवादित नेता बन गए हैं. कांग्रेस में विद्रोहियों का जो कथित जी-20 समूह था वो भी शांत हो गया है और सभी ने राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है.
भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी के नेता राहुल गांधी ही हैं.
इसके अलावा राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं में भी आगे निकल गए हैं. अब तक चाहे ममता बनर्जी हों या अरविंद केजरीवाल, वो सभी राहुल गांधी की गंभीरता पर सवाल उठाते रहे थे. आज उन सभी को लग रहा है कि राहुल गांधी के बिना विपक्ष की एकता मुमकिन नहीं है.
कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस यात्रा के ज़रिए सक्रिय हुए हैं. जिन-जिन राज्यों से ये यात्रा गुज़री है वहां पार्टी और कार्यकर्ता कार्यशील हो गए हैं. एक तरह से कहा जा सकता है इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को नई जान मिली है.
अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी या कांग्रेस को राजनीतिक रूप से कितना फ़ायदा होगा. लेकिन यदि कांग्रेस अब अपने दम पर सौ लोकसभा सीटने क स्थिति में भी पहुंच जाती है तो वो निश्चित रूप से विपक्ष का बड़ा चेहरा होंगे.
'राहुल ने साबित किया वो विपक्ष का केंद्र हैं'
राजकिशोर, वरिष्ठ पत्रकार
राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के उद्देश्य को लेकर घोषणा कुछ भी की हो, लेकिन निश्चित तौर पर इस यात्रा का मक़सद उन्हें राजनीतिक तौर पर स्थापित करना है.
जहां तक नफ़रत का माहौल दूर करने की बात है, तो कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक दल का परम उद्देश्य यही होना चाहिए. ये देश का मूल मुद्दा है, स्वस्थ समाज के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें किसी भी तरह की नफ़रत, वैमनस्य, छुआछूत या घृणा ना हो.
अगर कोई राजनीतिक दल इस तरह का उद्देश्य लेकर आगे चलता है तो सही ही है. इसमें कोई शक़ नहीं है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाया और लोगों को मिलकर एक साथ रहने का संदेश दिया.
राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का मक़सद सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर ही उन्हें गंभीर नेता के तौर पर स्थापित करने और उन पर पार्ट टाइम पॉलीटीशियन होने का जो आरोप लगता रहा है, उसे दूर करना था.
आज सवाल ये है कि पूरे देश में मोदी और बीजेपी के ख़िलाफ़ केंद्र कौन होगा, इस यात्रा से राहुल ने इसका जवाब देने की कोशिश की है. नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से उनके विरोधियों को भारत जोड़ो यात्रा ने पहली बार इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म दिया है.
भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही पहला काम ये किया कि कांग्रेस को विपक्षी दल का दर्जा ना देते हुए उसे क्षेत्रीय दलों से भी कमतर साबित करने और राजनीति में किनारे करने की कोशिश की.
राहुल गांधी के लिए सबसे अहम था कि देश की सबसे पुरानी और पहचान वाली पार्टी को पुनर्जीवित करना. भारत का शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जहां कांग्रेस पार्टी को लोग ना जानते हों.
विपक्ष में रह-रहकर क्षेत्रीय नेता सामने आ रहे थे. कभी ममता बनर्जी, कभी नीतीश कुमार, कभी केसीआर तो कभी अरविंद केजरीवाल. लेकिन इस यात्रा के ज़रिए राहुल ने ये साबित करने की कोशिश की है कि देश में सत्ता के विपक्ष का केंद्र वही हैं.
राहुल को पहले ख़ुद को स्थापित करना था कि देश में विपक्ष कांग्रेस के बिना नहीं हो सकता है.
जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी या संघ परिवार उसके विरोध का केंद्र होता था. अब कांग्रेस के सामने ये चुनौती थी कि वो अपने आप को विपक्ष का केंद्र बनाए. राहुल ने इस यात्रा से ऐसा ही किया है. राहुल अपनी इस कोशिश में बहुत हद तक कामयाब भी नज़र आ रही हैं.
यात्रा अब समाप्त हो गई है और राहुल गांधी बहुत से लोगों को अपने साथ लाने में कामयाब भी हुए हैं. हालांकि वो अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, केसीआर और ममता को साथ नहीं ला पाए.
लेकिन सवाल ये है कि विरोध किसने किया? आगे गठबंधन क्या शक्ल लेगा ये सीटों के बंटवारे पर निर्भर करेगा, लेकिन राहुल कम से कम ये साबित करने में तो कामयाब ही रहे हैं कि कांग्रेस का चेहरा वो हैं.
जितनी लंबी यात्रा राहुल गांधी ने की है वैसी यात्रा करना देश में किसी और दल के लिए संभव भी नहीं था. निश्चित तौर पर भारत की राजनीति में राहुल गांधी ने इस यात्रा से एक लंबी लकीर तो खींच ही दी है.
2012 में जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार हुई थी तब कांग्रेस ने एंटनी समिति बनाई थी. उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक तो नहीं हुई थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये पता चला था कि उस रिपोर्ट में कहा गया था कि कांग्रेस धर्म-निरपेक्ष दिखने की कोशिश में कई बार हिंदू विरोधी दिखने लगती है.
इसमें राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के कुछ बयानों का ज़िक्र था.
राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अपनी धार्मिक आस्था, अपनी मां सोनिया गांधी के विदेशी मूल और धर्म को लेकर उठने वालों सवालों पर हमेशा के लिए विराम लगा दें.
राहुल गांधी इस यात्रा में मंदिरों में गए, जनेऊ पहना, बार-बार भगवान का ज़िक्र किया, यानी राहुल गांधी ने अपने दर्शन का खुला प्रदर्शन करने की कोशिश की.
लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हिंदुत्व नरेंद्र मोदी की पिच है और इस पर मुक़ाबला करने में कांग्रेस कितना सफल हो पाएगी, इसे लेकर हमेशा सवाल रहे हैं. हिंदुत्व की पिच पर अभी कोई पार्टी बीजेपी की तरह नहीं खेल पाएगी. हालांकि अब बीजेपी राहुल पर उस तरह से हिंदू विरोधी होने का आरोप नहीं लगा पाएगी जैसा लगाती रही है.
और हिंदुत्व सिर्फ़ एकमात्र मुद्दा नहीं है. महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, ये भारत में अब भी बड़े मुद्दे हैं. बीजेपी लंबे समय से सत्ता में है, तो उसका कुछ स्वाभाविक विरोध भी होगा.
ऐसे में भले ही हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी बीजेपी को बहुत चुनौती ना दे पाएं, लेकिन बीजेपी अब राहुल गांधी को उस तरह हिंदू विरोधी साबित नहीं कर पाएगी जैसा कि करने में वो अब तक सफल रही थी. इस मामले में भले ही आंशिक रूप से, राहुल गांधी सफल तो रहे हैं.
भारत में हिंदुत्व को लेकर कई बयान आए हैं, हिंदू राष्ट्र को लेकर मांग भी उठी है, लेकिन क्या ये सरकार की तरफ़ से हो रहा है? इसका एक पहलू ये भी है कि आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मुसलमानों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है. बीजेपी और आरएसएस को ये समझ आ रहा है कि आप एक बड़ी आबादी को धर्म के आधार पर अलग नहीं कर सकते हैं.
देश में लोग नफ़रत और घृणा नहीं चाहते हैं. नफ़रत और घृणा के आधार पर देश या राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है. भारत अगर अंध धार्मिक राष्ट्रवाद की तरफ़ बढ़ेगा तो पाकिस्तान जैसा हो जाएगा, भारत कभी भी ऐसा बनना नहीं चाहता है.
कांग्रेस हो सकता है ये कहे कि ये राहुल गांधी की यात्रा का असर है. लेकिन ये सच है कि आरएसएस और बीजेपी अब मुसलमानों को अपनी तरफ़ खींचने का प्रयास करते दिख रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी पसमांदा मुसलमानों के लिए कार्यक्रम बना रही है.
बीजेपी मुसलमानों को अलग-थलग करने के आरोपों को ख़ारिज करने के प्रयास करती दिख रही है.

राहुल ने लोगों को जोड़ा लेकिन क्या वो वोट में बदल पाएंगे?
हेमंत अत्री, वरिष्ठ पत्रकार
इस यात्रा से सबसे पहली बात तो ये स्पष्ट हुई है कि अभी भारत में विपक्ष की जगह ख़त्म नहीं हुई है. विपक्ष की जगह अभी भी बरक़रार है, लेकिन विपक्ष को मज़बूत होने के लिए लोगों के बीच जाना होगा और उनसे बात करनी होगी.
पिछले आठ साल में एक तरह से बीजेपी मीडिया में हावी थी या बीजेपी का एकाधिकार था. मीडिया में बात बीजेपी से शुरू होकर बीजेपी पर ही ख़त्म होती थी. लेकिन राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए लोगों के बीच जाकर ये साबित कर दिया है कि विपक्ष भी अपनी जगह बना सकता है. आज सिर्फ़ क्षेत्रीय मीडिया ने ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय मीडिया ने भी राहुल गांधी की कवरेज की है और राहुल दिखाई देने लगे हैं.
राहुल की यात्रा से एक बात और स्पष्ट हई है कि लोग विपक्ष के साथ चलने को तैयार हैं. राहुल की यात्रा में भारी तादाद में लोग आए हैं, ये आगे चलकर वोट में बदलेंगे या नहीं ये भविष्य में पता चलेगा, लेकिन इस यात्रा ने बीजेपी के ख़िलाफ़ एक माहौल तो बनाया ही है.
भारत में बेरोज़गारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार के ख़िलाफ़ पहले से ही माहौल है. इस यात्रा में ये मुद्दे भी उठे हैं.
इस यात्रा का असर किसी एक राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में देखने मिला है. ये नहीं कहा जा सकता कि किसी राज्य में ये कमज़ोर रही है. इससे ये भी दिखा है कि अगर लोगों के बीच रहकर उनकी बात की जाए तो अपनी राजनीतिक ज़मीन भी मज़बूत की जा सकती है, और यही वजह है कि इस यात्रा को लेकर बीजेपी चिंतित है.
बीजेपी को चिंता इस बात की है कि आज जो ये माहौल बना है कल ये विपक्ष की एकजुटता की तरफ़ ना चला जाए. राहुल गांधी ने जुलाई में एक और यात्रा की योजना बनाई है. ये गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक जाएगी.
कांग्रेस ने इस यात्रा के ज़रिए देश में एक लहर पैदा की है. ऐसे में कांग्रेस के पास राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने का एकमात्र ज़रिया यही है कि इस मोमेंटम को आगे बनाए रखे. इसके लिए दूसरी यात्रा करना कांग्रेस की एक ज़रूरत भी होगी.
दूसरी वजह ये है कि आजकल चाहे पारंपरिक मीडिया हो या फिर मुख्यधारा का मीडिया, वो विपक्ष को जगह नहीं दे रहा है. अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए अब कांग्रेस के लिए ये और भी ज़रूरी हो गया है कि वो लोगों से सीधा संवाद करे.
इस भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं में जो जोश पैदा किया है उसे बनाए रखना भी पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है.
दूसरी यात्रा जुलाई में प्रस्तावित है जो गुजरात के सोमनाथ से शिलॉन्ग तक जाएगी. इस साल 9 राज्यों में चुनाव है, अगले साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होंगे. ऐसे में इस यात्रा का समय भी बहुत अहम होगा.
राहुल गांधी और कांग्रेस गुजरात में एक बहुत बड़ी ग़लती कर चुके हैं. उन्होंने गुजरात को थाली में रखकर बीजेपी को परोस दिया. राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य बड़े नेता गुजरात में प्रचार करने गए ही नहीं.
दूसरी यात्रा के दौरान या कुछ बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होंगे. पार्टी को ये भी तय करना होगा कि वो इन राज्यों में अपना अभियान कैसे चलाएगी.
एक चीज़ और स्पष्ट हुई है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है. साल 2019 के बाद कांग्रेस किसी राज्य में चुनाव नहीं जीती थी. लेकिन अब कांग्रेस ने हिमाचल में बीजेपी को हरा दिया है भले ही वो एक छोटा राज्य ही क्यों ना हो.
वहीं दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया है. इससे ये स्पष्ट हुआ है कि बीजेपी अपराजेय नहीं है. विपक्ष को स्थानीय मुद्दे उठाने होंगे, जनता से सीधे संवाद और संपर्क करना होगा और रणनीति से लड़ना होगा, ऐसा करके निश्चित रूप से बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है.
कांग्रेस पार्टी अगर राज्यों में अपने अंदरूनी मतभेद दूर करती है और इस मोमेंटम को बरकार रखते हुए चुनाव में जाती है तो निश्चित रूप से बीजेपी को चुनौती दे सकती है. हालांकि ये चुनौती कितनी बड़ी होगी और इसका चुनाव नतीजों पर क्या असर पडे़गा ये फ़िलहाल नहीं कहा जा सकता है.
आज़ादी के बाद से ये कांग्रेस का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान है. मीडिया ने कांग्रेस को कितनी जगह दी है सवाल ये नहीं है, तथ्य ये है कि कांग्रेस का संदेश आम लोगों तक पहुंचा है. कम से कम कांग्रेस लोगों तक अपनी विचारधारा और मुद्दों को लेकर तो गई है.
ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें राष्ट्रीय मीडिया नज़रअंदाज़ कर रहा है. जीएसटी, अदानी का कारोबार, नोटबंदी से हुआ नुक़सान, बेरोज़गारी, महंगाई.
ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राहुल गांधी सबसे प्रखर रहे हैं. भले ही पहले उन्हें 'पप्पू' कहकर ख़ारिज कर दिया गया हो, मीडिया ने उनकी बात को वो प्रथमिकता ना दी हो, लेकिन आज राहुल गांधी जब गंभीरता से ये मुद्दे उठा रहे हैं तो संदेश लोगों तक पहुंच रहा है. बीजेपी इसे ही लेकर चिंतित है.
'विपक्ष को एकजुट करने में नाकाम रहे राहुल गांधी'
उर्मिलेश, वरिष्ठ पत्रकार
राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी इस यात्रा का मक़सद नफ़रत के माहौल को ख़त्म करना है, सद्भावना पैदा करना है और भारत को जोड़ना है. लेकिन ऐसे राजनेताओं की यात्राओं का मक़सद राजनीतिक भी होता है.
जहां तक इस यात्रा के ज़रिए विपक्ष को जोड़ने का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी अभी तक इस यात्रा के ज़रिए विपक्ष को एकजुट करने में बहुत कामयाब नहीं हुए हैं. अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इस यात्रा के बाद क्या नतीजे निकलेंगे. कई बार ऐसा होता है कि कुछ घटना होती है और उस घटना के कुछ समय बाद चीज़ें स्वरूप लेती हैं. जहां तक वर्तमान का सवाल है, विपक्ष में बिखराव साफ़ नज़र आ रहा है.
कांग्रेस के जो संभावित सहयोगी हैं उनमें से कई तीस जनवरी को श्रीनगर नहीं पहुंच रहे हैं. कुछ ने स्पष्ट कर दिया है कि वो नहीं जा पा रहे हैं. कुछ ख़ामोश हैं. कांग्रेस ने 21 दलों को बुलाया है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि कुल कितने दल पहुंच रहे हैं.
संभावित विपक्षी सहयोगी दलों से हमने जानकारी लेने की कोशिश की थी कि कौन-कौन जा रहा है, लेकिन कोई बहुत सटीक या कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक जानकारी अभी तक नहीं मिली है.
विपक्ष दलों की अपनी-अपनी स्थिति और अपने-अपने कारण हैं, वहीं कांग्रेस की भी अपनी वजहें हैं. ये नहीं कहा जा सकता है कि एक तरफ से ही विपक्षी एकजुटता कमज़ोर हो रही है.
बीजेपी इस समय ताक़तवर है और उसके अपने समर्थक और राजनीतिक मशीनरी है. मीडिया भी बीजेपी के साथ है. वहीं विपक्ष अभी भी बिखरा हुआ है. इन परिस्थितियों में विपक्ष के लिए एकजुट होना बहुत ज़रूरी है.
अब तक जब-जब केंद्रीय सत्ता का बदलाव हुआ है, ख़ासकर जब केंद्र में ताक़तवर सत्ता रही है, चाहें वो फिर इंदिरा गांधी का दौर हो या फिर राजीव गांधी की या कोई और सरकार रही हो, यहां तक वाजपेयी की सरकार भी तब ही बदली थी जब विपक्षी दलों ने मोर्चेबंदी की और एक साझा एजेंडे को आगे बढ़ाया या फिर आंदोलन या अभियान चलाया. इसके बिना जनता एकजुट नहीं हो पाती है.
कई बार जब जनता अपने मुद्दों को लेकर सत्ता के विरोध में भी होती है तब भी वो विपक्ष में बिखराव की वजह से समझ नहीं पाती है कि सत्ता के ख़िलाफ़ किसे वोट करे. यही विखराव सत्ताधारी दल के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है.
कभी विपक्ष में बिखराव की वजह से कांग्रेस जीता करती थी, आज बीजेपी जीत रही है. बीजेपी को अगर देखा जाए तो देश के बड़े हिस्से में उसका मज़बूत आधार नहीं है लेकिन फिर भी वो जीत रही है. बड़ी संख्या में सीटें लेकर आ रही है क्योंकि विपक्ष में बिखराव है.
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात को छोड़कर बीजेपी कहीं कोई ऐसी बड़ी ताक़त नहीं है जहां उसे चुनौती ना दी जा सके. कर्नाटक में भी अभी उसे चुनौती मिल ही रही है.
ऐसे में विपक्ष अगर एकजुट होता है तो केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी को चुनौती दे सकता है. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष को एकजुट करने का एक बड़ा ज़रिया हो सकती थी. लेकिन ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी अभी तक विपक्ष को अपने प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं ला सके हैं.
वीपी सिंह जब नेता बन रहे थे, तब किसी को नहीं पता था कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन वो विपक्ष के अभियान का नेतृत्व कर रहे थे और नेतृत्व करने के कारण ही वो प्रधानमंत्री बने. आज ज़रूरत ये है कि विपक्ष के अभियान का कोई नेतृत्व करे. सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी विपक्ष का कोई अभियान छेड़ पाते हैं और उसका नेतृत्व कर पाते हैं?
'पार्टी की अंदरूनी कलह दूर करने में नाकाम रहे राहुल गांधी'
राधिका रामासेषन
भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने इसके ज़रिए जो मोमेंटम पैदा किया है उसे वो साल 2024 तक बरक़रार रख पाएंगे. इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए अपनी छवि को बदला है.
वो एक गंभीर राजनेता के रूप में स्थापित हुए हैं. बहुत कट्टर भाजपा समर्थकों को छोड़कर अब कोई उन्हें पप्पू नहीं कहता है. बीजेपी ने उनकी जो एक छवि बनाई थी वो अब टूट गई है.
ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उनकी छवि को बदलने में कामयाब रही है. लेकिन अब भी सवाल यही है कि क्या ये बदली हुई छवि मतदाताओं को आकर्षित करेगी?
लोकसभा चुनाव में अभी क़रीब डेढ़ साल है. ऐसे में सवाल ये भी है कि राहुल गांधी डेढ़ साल तक क्या इस जोश को बरक़रार रख पाएंगे?
कांग्रेस इस समय कई राज्यों में अंदरूनी रूप से बंटी हुई है. उदाहरण के तौर पर राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच प्रतिद्वंदिता खुलकर सामने आ गई है.
भारत जोड़ो यात्रा चल ही रही थी कि सचिन पायलट ने एक तरह से राजस्थान में अपनी अलग यात्रा शुरू कर दी. वो जगह-जगह जा रहे हैं और बैठकें कर रहे हैं. उन्होंने अशोक गहलोत को लेकर कुछ टिप्पणियां भी की हैं.
वहीं अशोक गहलोत पत्रकारों से सचिन पायलट को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं. राजस्थान राहुल गांधी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है.
ऐसी ही चुनौती पंजाब में है. पंजाब में लोग आम आदमी पार्टी की सरकार से बहुत ख़ुश नहीं है. लेकिन क्या कांग्रेस उसका फ़ायदा उठा पा रही है? ऐसा दिख नहीं रहा है.
वहीं हिंदी पट्टी में भी कांग्रेस अपनी पहचान मज़बूत नहीं कर पा रही है. बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ जुड़ी है, वहां अपनी अलग पहचान नहीं बना पा रही है. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मज़बूत करने का कोई प्रयास होता नहीं दिख रहा है.
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी ज़रूर मज़बूत होती दिख रही है, लेकिन राजस्थान में स्थिति कांग्रेस के हाथ से निकलती दिख रही है. ऐसे में सिर्फ़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ही कांग्रेस को कुछ उम्मीदें होंगी.
वहीं दक्षिण भारत में कांग्रेस हमेशा से मज़बूत रही थी.आपातकाल के बाद जो चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस दक्षिण में ही कुछ सीटें जीत पाई थी. ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को भारत जोड़ो से दक्षिण भारत में कुछ फ़ायदा हो सकता है. कर्नाटक में कांग्रेस मज़बूती से लड़ सकती है.

कर्नाटक राहुल गांधी के साथ सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार
कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच मनमुटाव के कुछ कम होने की भी रिपोर्टें मिल रही हैं. लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस वहां अपने इस मोमेंटम को बरक़रार रख पाएगी. मई में वहां चुनाव होने हैं, ऐसे में जल्द ही इसका पता चल पाएगा.
केरल में पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था. इस बार भी कांग्रेस को उसे दोहराना होगा. लेकिन वहां शशि थरूर एक फ़ैक्टर हैं. कई बार वो ऐसे बयान देते हैं जिनसे कांग्रेस संतुष्ट नहीं होती है. सवाल ये भी है कि क्या राहुल केरल में पार्टी के संगठन को सुधार पाते हैं?
वहीं तेलंगाना में राहुल की यात्रा में भारी भीड़ जुटी. लेकिन यात्रा के वहां से निकलने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के ख़िलाफ़ प्रतिरोध हो गया. यात्रा निकलने के कुछ समय बाद ही वहां अध्यक्ष के ख़िलाफ़ बग़ावत हो गई. भारत जोड़ो यात्रा का मक़सद कांग्रेस के संगठन को भी जोड़ना था. लेकिन तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के निकलते ही संगठन में बिखराव हो गया. तेलंगाना का घटनाक्रम हैरान करता है.
राहुल को फ़िलहाल सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के भीतर से मिलती दिख रही है. पार्टी को मज़बूत करना उनकी ज़िम्मेदारी है. इसमें कोई शक़ नहीं है कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के ज़रिए अपनी साख बनाई है और सहानुभूति हासिल की है, लेकिन अब उनका काम इस साख को वोट में बदलने का होगा. सवाल अब भी यही है कि क्या वो ऐसा कर पाएंगे?
राहुल ने पार्टी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है, सोशल मीडिया पर भी पार्टी अधिक सक्रिय हुई है, लेकिन अब भी कांग्रेस की इस मामले में बीजेपी से कोई तुलना नहीं की जा सकती है. बीजेपी का संगठन कांग्रेस से कई गुना मज़बूत है.
उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठनात्मक रूप से बहुत मज़बूत है. बीजेपी की अपनी पार्टी तो है ही इसके अलावा लगभग 45 संगठन ज़मीन पर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं. ये बेहद सक्रिय हैं. वहीं दूसरी तरफ़ कांग्रेस के पास ऐसा ढांचा नहीं है.
एनएसयूआई या सेवादल यूपी में ज़मीन पर कहीं नज़र नहीं आते हैं.
राहुल गांधी जब यात्रा कर रहे थे तो पार्टी के लोग उनके साथ चल रहे थे, तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे, इससे पार्टी संगठन में कुछ जान तो आई है, लेकिन ये इतनी नहीं है कि अभी बीजेपी से मुक़ाबला कर सके.
राहुल गांधी इस समय संगठन की पूरी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ मल्लिकार्जुन खड़गे पर नहीं छोड़ सकते हैं. उन्हें बीजेपी की तरह लगातार कार्यक्रम करने होंगे ताकि उनके कार्यकर्ता सक्रिय रहें और अपने समर्थकों और मतदाताओं के साथ जुड़ने के प्रयास करते रहें.
कांग्रेस को कुछ नए कार्यक्रमों के बारे में सोचना होगा ताकि भारत जोड़ो यात्रा से पैदा हुए जोश को आगे बरक़रार रखा जा सके, अन्यथा इसे ठंडा होने में बहुत दिन नहीं लगेंगे.

'राहुल की छवि तो सुधरी, लेकिन बीजेपी को नुक़सान नहीं'
प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार
भारत जोड़ो यात्रा का एक मक़सद था राहुल गांधी की छवि का मेकओवर करना. कम से कम इसमें ये यात्रा अब तक सफल रही है.
जहां तक बीजेपी को चुनौती देने की बात है. दो चीज़ों की ज़रूरत है. पहला तो संगठन और दूसरा वैकल्पिक राजनीतिक विमर्श. आज की स्थिति में कांग्रेस में इन दोनों का अभाव दिखता है.
सवाल ये है कि लोग अगर बीजेपी को हटाकर कांग्रेस को सत्ता में लाएं तो क्यों लाएं? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए इस सवाल का जवाब नहीं दे सके हैं.
अगर जनता मोदी और बीजेपी को हटाती है और कांग्रेस और राहुल गांधी को लाती है तो वो क्या नया करेंगे ये वो अभी तक जनता को नहीं समझा सके हैं. जनता जब तक इस सवाल पर संतुष्ट नहीं होगी वो बीजेपी को किसी तरह की चुनौती नहीं दे पाएंगे.
जब तक राहुल गांधी जनता की विश्वसनीयता हासिल करेंगे तब तक भारत जोड़ो यात्रा या किसी भी अन्य कार्यक्रम का असर नहीं होगा. इस यात्रा से ये ज़रूर हुआ है कि कांग्रेस पिछले चार महीने से चर्चा में हैं. निश्चित रूप से इससे राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ है.
राहुल गांधी ने तमिलनाडु से ये यात्रा शुरू की थी और वो कश्मीर पहुंचे हैं. सवाल ये है कि क्या इससे पार्टी के संगठन को कोई फ़ायदा हुआ. केरल में पार्टी में अंदरूनी कलह चल रही है, तेलंगाना में भी नेतृत्व को लेकर विवाद है, राजस्थान में भी खुला मतभेद है.
ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी में कोई एकजुटता आई हो. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी में जगह-जगह मतभेद दिखाई पड़ी है. ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि इस यात्रा के बाद भी कांग्रेस बीजेपी को राजनीतिक चुनौती दे सकेगी.
अभी तक इस यात्रा का हासिल सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि लोग राहुल गांधी की बात सुनने लगे हैं. लेकिन अभी ये होता नहीं दिख रहा है कि लोग राहुल गांधी की बात मान रहे हैं.
राहुल गांधी ने ये यात्रा तमिलनाडु से शुरू की. कांग्रेस डीएमके की सहयोगी है इसलिए इसमें एमके स्टालिन शामिल हुए. उनके अलावा फारूख़ अब्दुल्ला इस यात्रा में शामिल हुए हैं. इन दोनों नेताओं को छोड़ दिया जाए तो क्षेत्रीय दल का कोई ऐसा बड़ा नेता इस यात्रा में शामिल नहीं हुआ है जो बीजेपी के ख़िलाफ़ हो.
जो दल यूपीए के सदस्य हैं, जैसे आरजेडी है, नीतीश कुमार यूपीए में नहीं हैं, लेकिन महागठबंधन में हैं. महाराष्ट्र के शरद पवार या उद्धव ठाकरे, दोनों कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन वो शामिल नहीं हुए, अपने बच्चों को उन्होंने यात्रा में भेजा.
अगर इस यात्रा से राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आता दिख रहा होता तो विपक्षी दलों में भरोसा बढ़ता कि हम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं और हमें उसके साथ खड़े होना चाहिए. लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है.
राहुल गांधी देश में नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत फैलाने की बात करते हैं. राहुल गांधी ने जब यात्रा शुरू की थी तब उन्होंने कहा था कि 'देश में नफ़रत है और मैं मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं.'
क़रीब तीन हज़ार किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने दिल्ली में कहा कि मैं तीन हज़ार किलोमीटर चला हूं और मुझे देश में कहीं नफ़रत नहीं दिखाई दे रही है. यानी राहुल गांधी ने ख़ुद अपनी ही बात को काट दिया. राहुल गांधी ये दावा करते रहे हैं कि देश में नफ़रत है, लेकिन जब उन्हें ही नफ़रत नहीं दिखी तो फिर नफ़रत है कहां? (bbc.com/hindi)
-प्रकाश दुबे
हॉकी की बदहाली पर सिर्फ रोना रोने वाले चकित हैं। शर्मिंदा हों न हों। सरकारी फाइलों में बेअसर हॉकी की मार को नए ब्रांड एंबसडर ने देश को आजाद कराने वाले नारे से जोड़ा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारा था-करो या मरो। जीतने वाले या वोट दिलाऊ शोहरत पाने वाले कलाकार-खिलाड़ी को ईनाम बांटने का रिवाज पुराना है। इस नारे को ओडिशा सरकार ने हॉकी को चमकाया। पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पार्टी उम्मीदवार बनाकर राज्यसभा भेजा। 85 अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी देने वाले आदिवासी बहुल जिले सुंदरगढ़ में शानदार हॉकी स्टेडियम बना। विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता जारी है। नवीन बाबू को गांवों से प्रेरणा मिली। सुंदरगढ़ जिले की दिलचस्प परंपरा है। बच्चे करो या मरो की भावना से हॉकी खेलते हैं। जीतने वाले बच्चों को सरकार या बाकी कोई कुछ दे या न दे, गांव वाले मुर्गा या बकरा ईनाम देते थे। जितनी बड़ी जीत। उतने अधिक बकरे। जीत की चाह जगाने में बकरों की बलि से भी सरकारें सबक ले सकती हैं।
सविनय अवज्ञा आंदोलन
भारत जोड़ो की पुलिस सुरक्षा में कश्मीर और दिल्ली के रहनुमा सर खपाते रहें। हमसे सुनो हवाल इन दिनों केन्द्रशासित जम्मू-कश्मीर में जारी अजीब किस्म का सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 22 दिसंबर 2022 को फरमान जारी हुआ था कि सारे सरकारी कर्मचारी 31 जनवरी 2023 तक सालाना अपनी संपत्ति का ब्यौरा आन लाइन भिजवा दें। गणतंत्र दिवस बीत गया। कर्मचारियों की नाफरमानी का आलम यह है कि प्रशासन को फिर से कड़ा निर्देश जारी करना पड़ा। चेतावनी दी गई कि अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी और उसके बाद आन लाइन विवरण लेना बंद होगा। सतर्कता विभाग, वेतन विभाग आदि नाफरमानी करने वालों को देख लेंगे। इससे जुड़ी दूसरी विपदा। एक अप्रैल से संपत्ति कर लागू करने का शहरी विकास मंत्रालय का पक्का इरादा है। जम्मू कश्मीर के आवास और शहरी विकास विभाग के अफसरों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। वज़ह भारतीय जनता पार्टी भी प्रस्ताव का विरोध कर रही है। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर दबाव है कि सिर्फ कारोबारी इमारतों से संपत्ति कर वसूलें। घरों का छूट मिले।
नमक कानून
गणतंत्र दिवस पर अलंकरण से सजने वाले बधाई के पात्र हैं। एक से अधिक बधाई के पात्रों में दो पुलिस अधिकारी शामिल हैं। देवेन भारती ने पांच जनवरी को मुंबई के विशेष पुलिस आयुक्त का प्रभार संभाला। यह पद पहली बार बना। भारती के विरुद्ध जांच और प्राथमिकी कचरा टोकरी में गईं। जांच करने वाले पुलिस महानिदेशक संजय पांडे जमानत पर घर बैठे। राष्ट्रपति से पुलिस पदक पाने वालों की सूची में नाम दर्ज हुआ।
महानिदेशक की दौड़ में फिलहाल रश्मि शुक्ला से पीछे हैं। दूसरा नाम जम्मू कश्मीर के विजय कुमार का है। जवाहर लाल नेहरू विवि में पढ़ाई के कारण सीखे दांवपेंच के कारण विजय कुमार को नक्सली गंठजोड़ तोडऩे के लिए बस्तर में तैनाम किया गया था। अमित भाई की टीम उन्हें दिल्ली में चाहती है। जम्मू कश्मीर कैडर का होने के कारण पुलिस महानिदेशक के लिए दावा तो बनता ही है। विजय कुमार को 2022 में महानिरीक्षक से पदोन्नत किया गया। उनके छप्पन इंच के सीने पर राष्ट्रपति का पुलिस पदक सजेगा। वैसे पदक संख्या में उनसे होड़ लेने वाला शायद ही कोई दूसरा पुलिस अधिकारी हो।
खिलाफत
महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वसंतपंचमी को अपना जन्मदिन मनाते थे। वर दे वीणावादिनि, वर दे कविता लिखने वाले निराला का जन्म बंग भूमि महिषादल में हुआ। हाथे खड़ी पर्व पर सरस्वती पूजा के साथ अक्षर ज्ञान की शुरुआत होती है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनकर पहुंचे बोस के नाम से सुभाष चंद्र बोस का भ्रम होगा। आनंद बोस मलयाली हैं। पिछले सालों का तनाव खत्म करते हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री हाथे खड़ी समारोह में साथ साथ थे। राज्यपाल ने बांग्ला अक्षर लिखा और राज्यपालों के प्रति दुर्गावतार धारण करने वाली ममता बनर्जी ने मधुर वाणी में मलयालम में अभिवादन किया। भाषा संगम हो और खिलाफत न हो? ऐसा नहीं हो सकता। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ममता-मोह से परे हैं। नेताजी सुभाष बाबू पर श्रद्धा है। राज्यपाल बोस पर कुपित हैं। लोकसभा सदस्य दिलीप बाबू का कहना है कि बच्चों के अक्षर ज्ञान कार्यक्रम तमाशे में राज्यपाल को जाने की जरूरत नहीं थी।
विशेष- सभी शीर्षक महात्मा गांधी के जन आंदोलनों के नाम हैं।
(लेखक दैनिक भास्कर नागपुर के समूह संपादक हैं)
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पृष्ठ पलटकर सारे देश को दिखा दिया है। उन्होंने ‘केरल हिंदू आॅफ नार्थ अमेरिका’ नामक संस्था को संबोधित करते हुए कहा कि प्रसिद्ध मुस्लिम नेता और बड़े चिंतक सर सय्यद अहमद खान ने अब से लगभग डेढ़ सौ साल पहले आर्यसमाज की एक सभा में यह बात दो-टूक शैली में कही थी कि उन्हें अपने आप को हिंदू कहने में जरा भी संकोच नहीं है। उन्होंने सभी श्रोताओं से कहा कि आप चाहें तो मुझे हिंदू ही कहें, क्योंकि जो आदमी भारत में पैदा हुआ है, जो व्यक्ति यहां का अन्न खाता है और यहां की नदियों का पानी पीता है, वह हिंदू नहीं है तो कौन है? उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द का धार्मिक अर्थ निकालना गलत है।
हिंदू शब्द तो शुद्ध भौगोलिक है। हिंदू शब्द की व्याख्या करते हुए यही बात मैंने अपने ग्रंथ ‘‘भाजपा, हिंदुत्व और मुसलमान’’ में विस्तार से प्रतिपादित की है। सच्चाई तो यह है कि हिंदू या हिंदुत्व शब्द भारत के किसी भी धर्मग्रंथ में नहीं है। मैंने वेद, उपनिषद्, दर्शन ग्रंथ और पुराण ग्रंथ भी पढ़े हैं। इन सभी ग्रंथों में यहां तक की रामायण और महाभारत में भी हिंदू शब्द कहीं नहीं आया है। भारत के निवासियों के लिए प्रायः आर्य शब्द का ही प्रयोग होता रहा है। वास्तव में हिंदू शब्द का प्रयोग अरब और फारस के मुसलमानों ने पहली बार किया है। वास्तव में हिंदू शब्द के इस्तेमाल की उत्पत्ति हम खोजने लगें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि यह इस्लामी शब्द है लेकिन इसका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। यह मजहबी नहीं, भौगोलिक शब्द है। हिंदू शब्द सिंधु से बना है। फारसी भाषा में ‘स’ का उच्चारण ‘ह’ होता है। सिंधु को फारसी भाषा में ‘हिंदू’ कहते हैं। सिंधु नदी के इस पार जो लोग रहते हैं, उन्हें हिंदू कहा जाता है। यह हिंदू शब्द चीन में ‘इंदु’ बोला जाता है। मैं चीन के गांवों में जाता था तो चीनी लोग चीनी भाषा में कहते थे कि ‘मैं इंदू हूं’, क्योंकि मैं ‘इंद’ से आया हूं। एक बार मेरे साथ शांघाई में कुछ मुंबई के मुसलमान मित्र भी बाजार में घूम रहे थे। उन्हें भी चीनी लोग ‘इंदु रैन’ याने हिंदू आदमी ही बोल रहे थे। दूसरे शब्दों में हर भारतीय हिंदू ही है। उसे विदेशों में अलग-अलग उच्चारणों से जाना जाता है। उसे ‘हिंदी’, ‘हिंदवी’, ‘हून्दू’, ‘हन्दू’, ‘इंदू’, ‘इंडीज़’, या ‘इंडियन’ भी कह दिया जाता है।
मेरी इस हिंदू शब्द की व्याख्या को आरिफ भाई ने सर सय्यद की मोहर लगाकर और अधिक प्रामाणिक बना दिया है। स्वयं आरिफ भाई बड़े विद्वान नेता हैं। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने पिछले दिनों कई बार इस कथन को दोहराया है कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक ही है। इसीलिए हमारी मुसलमान मोहम्मदी हिंदू हैं और हमारे ईसाई मसीही हिंदू हैं। यही भाव भारत की एकता को सबल बना सकता है। हमारे मुसलमानों और ईसाइयों को मैं इसीलिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मुसलमान और सर्वश्रेष्ठ ईसाई कहता हूं, क्योंकि उनकी रग-रग में हजारों वर्षों का भारतीय संस्कार जिंदा बहता है। (नया इंडिया की अनुमति से)
आज भी गांधी यादों की किरकिरी हैं। देश के करोड़ों नौजवान बेकार हैं। उनकी शिक्षा को मस्तिष्क से घुटनों की ओर यात्रा कराई जा रही है। अमीर परिवारों में कम से कम एक सदस्य को विदेश भगाया ही जा रहा है। नेता और उद्योगपति गंभीर बीमारियों में विदेश जाकर ही मरना चाहते हैं। झूठ, फरेब, झांसा, धोखा पीठ पर वार, चुगली, अफवाह सबका बाजार सेंसेक्स पर काॅरपोरेटिए उछलवा रहे हैं। वे ही देश के मालिक हैं। गांधी नहीं जानते थे नेता आगे चलकर काॅरपोरेटियों की कठपुतलियों की तरह अभिनय करेंगे। बुद्धिजीवी जीहुजूरी की धींगामस्ती करते वजीफा, पद और पद्म पुरस्कार पाएंगे। किसानों को आत्महत्या ब्रिगेड में बदला जाएगा। महिलाएं सड़कों से लेकर दफ्तरों और धर्म संस्थानों में भी देह बनाकर कुचली जाएंगी। अफसर खुद को गोरों की जगह गेहुंआ अंगरेज कहेंगे। सब मिलकर गांधी को इत्मीनान था कि साल में दो दिन जबरिया आए मेहमान की तरह लोग उन्हें बेमन से हाय हलो करेंगे। फिर अगले दिन इतिहास की गुमनामी की पगडंडी पर जाता देख मुस्कराकर टाटा करते रहेंगे। त्रासद यही है कि गांधी जिन्न नहीं हमारी जिंदगी हैं। इसलिए मरते भी नहीं हैं।
गांधी तो आज़ादी के वर्षों पहले से ही बिकाऊ तक नहीं बचे थे। दिल्ली के तख्ते ताऊस पर उनके चेले विराज रहे थे। वे नोआखाली की गलियों में हिन्दू मुसलमान के सड़ते घावों पर मरहम बनकर घर-घर रिस रहे थे। भारत की संविधान सभा में मुल्क की इबारत लिखने में गांधी की खड़िया हाथों से छिटक गई थी। आज़ादी की दहलीज़ पर गांधी अपशकुन की तरह आकर खड़े हो ही गए। तो एक स्वयम्भू सांस्कृतिक राष्ट्रवादी ने बन्दूक की उंगलियाँ उनकी छाती में धँसाकर खून पी लिया। गांधी का चरखा बेहद पिछड़ा, दकियानूस और ढीला ढाला होने से उसका राजघाट से विसर्जन कर दिया गया। शराबबंदी के वे प्रणेता थे। पार्टी संविधान में शराबबंदी की शर्त चिपकी बैठी थी, लेकिन टिकट उसे मिलती जो ज्यादा पी सके। शराब ठेकेदार प्रदेश अध्यक्ष बनते और दलाल जिलाध्यक्ष। ग्राम स्वराज का सपना कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। आखिरी व्यक्ति के आँसू पोंछने का गांधी ताबीज बाँटते फिरते थे। वह आदमी इन्सान होने की परिधि से छिटककर पशुओं की तरह जुल्म सह रहा है। अंग्रेज़ सभ्यता को गांधी ने कोढ़ कहा था। उनके ही सत्ता-वंशजों ने सफेदी की तरह देह पर मल लिया। वे चाहते थे कि हमारे हुक्मरान तोप, तमंचों और बन्दूक-संगीनों के पहरों में नहीं रहें। हमारे पाँच सालाना राजनीतिक खसरों के अलग-अलग रकबाधारियों ने अंगरेज़ों से ज्यादा सुरक्षाकर्मी अपने चारों ओर बाड़ की तरह उगा लिये ताकि वे खेत को हिफाजत से चर सकें।
खादी की आधी टांगों पहनी धोती, कमर खुसी घड़ी, अजीब तरह के फ्रेम की ऐनक लगाए गांधी बिल्कुल वैसे दिखते हैं जैसे कि वे हैं ही। गांधी अधबुझे कोयले पर पड़ी सफेद राख की तरह दिखते हैं। फूंक मारकर उनके ताप और रोशनी को देखा और महसूस किया जा सकता है। इस अर्थ में गांधी हरीकेन का मानव रूप हैं। वे लगातार अपनी सात्विक जिद के सत्याग्रही हथियारों सिविल नाफरमानी और असहयोग को अंगरेजी सल्तनत को ढहाने करोड़ों मुफलिसों, अशिक्षितों, कमजोरों, पस्तहिम्मतों को हमकदम कर लेते हैं। बीसवीं सदी की राजनीति में ऐसा अजूबा बस केवल एक बार यही तो हुआ। जानना दिलचस्प है अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा अपने सीनेट कार्यालय में गांधी का एक बड़ा चित्र प्रेरणा पुरुष की तरह लगाते हैं।
गांधी क्लास को थर्ड क्लास का समानार्थी कहता हिकारत भरा अज्ञानी जुमला गांधी पर चस्पा कर दिया जाता है। गांधी ने बैरिस्टरी पढ़ते रोमन लाॅ के पर्चे को हल करने के लिए लेटिन भाषा ही सीख ली। अंगरेजी गद्य में उनकी ऐसी महारत रही है कि यदि राजनीति के पचड़े में नहीं भी पड़ते, तो केवल लेखन के इतिहास में हिन्दुस्तान क्या देश के बाहर भी सबसे बड़े गद्यकारों में शामिल होते। गांधी में बुद्धिजीवी विचार एक वृक्ष की तरह विकसित नहीं होता तो संभव है दुनिया के कई संघर्षशील जननेताओं की तरह गांधी भी इतिहास के बियाबान में केवल याद होते रहने के लिए दफ्न हो जाते।
स्वैच्छिक सादगी का आह्वान करने वाले गांधी शुरुआती जीवन में अंगरेजी वस्त्रों और भौतिक सुविधाओं से लैस रहे हैं। धीमी गति का पाठ पढ़ाने वाले गांधी के जीवन में इतनी तेज़ गतिमयता रही है कि वह भारत में किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति में देखने को नहीं मिलती। स्वैच्छिक गरीबी का उनका उद्घोष अलबत्ता उनके जीवन में प्रदर्शित रहा। अंगरेजी पार्लियामेन्ट को शुरू में वेश्या और बांझ कहने वाले गांधी भारतीय जीवन को उसी संसदीय पद्धति से बचा नहीं पाए। इस निर्णय को जनमानस का हुक्म होने के नाते उन्होंने स्वीकार कर लिया।
संसार में केवल गांधी बोले थे कि रोज़ अपने को सुधारते हैं। पीढ़ियां और इतिहासकार उनकी आखिरी बात को सच मानें। विपरीत, विसंगत और विकृत विचारों के किराए के भाषणवीर खुद के मन से बासी विचारों की सड़ांध बाहर नहीं निकालते। आज होते तो लुटते आदिवासियों के साथ खड़े होकर गोली भी खा सकते थे। उनका अठारह सूत्रीय रचनात्मक कार्यक्रम दफ्तर के कूड़े के डिब्बों में डाल चुके मंत्री गांधी प्रवक्ता बने अखबारों के पहले पृष्ठ पर विज्ञापित होते टर्रा रहे हैं। इलेक्ट्राॅनिक मीडिया में गांधी विरोधी उनकी विचारधारा का मुंह नोच रहे हैं। गांधी अपनी मातृभूमि की ऐतिहासिकता की नीयत थे। उनके सियासी, प्रशासनिक, वैचारिक वंशजों ने उन्हें मुल्क की नियति नहीं बनाया। जश्नजूं भारत फिर भी गांधी के नाम पर इतिहास को लगातार गुमराह करते रहने से परहेज़ नहीं करेगा क्योंकि उसे आइन्स्टाइन की भविष्यवाणी को सार्थक करना है कि आने वाली पीढ़ियां कठिनाई से विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस का ऐसा कोई व्यक्ति धरती पर कभी आया था।
गांधी ने अपनी पत्नी, पुत्र, बहन सबको दुख दिया। लोकतांत्रिक थे जो मर्यादा भुजा उठाए अपनी भावनाओं की हत्या करते रहे। परिवारजनों ने अछूत और कुष्ठ रोगियों का मलमूत्र साफ करने से इनकार कर दिया था तो उन्होंने रिश्तों को ही कुचल दिया। महात्मा की देह में पसीने की बदबू रोज विस्तारित होती थी। उनकी बहती छाती के रक्त के कण कण में राम का नाम गूंजता था। गांधी को हरिजन नाम प्रिय था। वह भी उनसे छीन लिया गया। वह जीवन भर बकरी का चर्बी रहित दूध पीते रहे। उनके जन्मस्थान पोरबन्दर के नाम पर घी के व्यापारियों की तोंदें फूल रही हैं। वे गरीबों की लाठी टेकते अरब सागर में नमक सत्याग्रह करते रहे। उनकी याद में दांडी नमक बेचते व्यापारी अरबपति हुए जा रहे हैं। गांधी के बेटों के शरीर का नमक घटता जा रहा है, लेकिन चेहरे की चाशनी बढ़ती जा रही है।
-जगदीश्वर चतुर्वेदी
इन दिनों आत्मकथा पर बहुत बातें हो रही हैं, लेखक-लेखिकाएं आत्मकथा लिखने में व्यस्त हैं, आत्मकथा की परंपरा और विधागत संस्कारों को अधिकतर आत्मकथा लेखक जानते ही नहीं हैं, उनके आत्मकथा लेखन में निजी जीवन इस कदर छाया हुआ है कि आपको लेखक का समकालीन समाज और इतिहास नजर ही नहीं आएगा। आत्म में एकदम लीन होकर लिखी गयी आत्मकथाएं वस्तुत: आत्म का छद्म निर्मित करती हैं, इस तरह की आत्मकथाएं न तो लेखक पर रोशनी डालती हैं और न समाज पर ही रोशनी डाल पाती हैं। लेखक अपने घर-परिवार की चौहद्दी में इस कदर मशगूल नजर आता है कि उसमें प्रेरणा लायक बहुत कम अंश नजर आते हैं। आत्मकथा का स्व और समाज से द्वंद्वात्मक संबंध है, इस संबंध का स्व के साथ ऐतिहासिक रिश्ता है जिसे आजकल के लेखक देखना पसंद नहीं करते।इसके चलते आत्मकथा महज आत्म प्रपंच और आत्मश्लाघा है।
हिन्दी के मध्यकालीन उर्दू कवियों में आत्मकथा लेखन की परंपरा के अनेक प्रमाण नजरों से गुजरे हैं, इनमें मीर तकी ‘मीर’की आत्मकथा ‘जिक्रे-मीर’ का नाम खासतौर पर उल्लेखनीय है। व्यक्ति, परिवार, समाज, राजसत्ता आदि के अन्तर्विरोधों और संघर्षों का इसमें विशद विवेचन मिलता है। यह आत्मकथा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उत्तर भारत के मुगलकालीन पतन के दौर में मराठों, जाटों, अंग्रेजों, पठानों के संघर्षो का अछूता पक्ष सामने आता है,साथ ही मुहम्मदशाह की मृत्यु से लेकर गुलाम कादिर रुहेला के अत्याचारों की दास्तां बयां की गई है। इसमें मीर के जीवन के तमाम अनछुए पहलू भी सामने आते हैं। मेरे ख्याल से आत्मकथा विमर्श में मीर की आत्मकथा हम सबकी मदद कर सकती है,हम कैसे आत्मकथा लिखें , हम यह सीख सकते हैं।
मीर मुहम्मद तक़ी ‘मीर’ (1709-1809) का उपनाम ‘मीर’ था।ठीक सौ साल जिन्दा रहे। आगरा में 1709 में पैदा हुए और 1809 में लखनऊ में मौत हुई। इस दौरान तकरीबन 65 साल दिल्ली में रहे। बेहद स्वाभिमानी, निस्वार्थी और कष्ट सहिष्णु शायर के रूप में मशहूर थे।भयानक गरीबी में जिंदगी गुजारी लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं पसारा। उर्दू कविता में नई भाषा,नए विषय और नई शैलियों को जन्म देने वाले इस महान शायर का लोहा गालिब और जौक भी मानते थे।
रेख़्ते के तुम्हीं उस्ताद नहीं हो गालिब।
कहते हैं अगले जमाने में कोई’मीर’ भी था।
‘मीर’के स्वभाव की तीन बड़ी कमजोरियां थी, पहली वे तुनकमिजाज थे, दूसरे रूखे स्वभाव के थे और तीसरे दुनियादारी से अनभिज्ञ थे। दूसरों की प्रशंसा करने में कंजूसी से काम लेते थे। जरा-जरा सी बात पर उनके दिल को ठेस लग जाती थी। जो दिल में आता वैसा ही कह देते थे। इसके कारण उनकी तकलीफें और बढ़ गयीं। एक दिलचस्प किस्सा है।
जब दिल्ली से लखनऊ को प्रस्थान किया तो उनके पास बैलगाड़ी का भाड़ा नहीं था। अत:एक यात्री को साझीदार बनाकर यात्रा आरंभ की। रास्ते में यात्री ने बात करने की कोशिश की तो ‘मीर’ साहब ने जवाब नहीं दिया और मुँह फेरकर बैठ गए। कुछ देर बाद उस यात्री ने फिर बात करने की कोशिश की तो ‘मीर’ साहब ने पलटकर तेवर के साथ कहा ‘बेशक, आपने किराया दिया है।आप गाड़ी में शौक से बैठे चलें, मगर बातों से क्या ताल्लुक?’
यात्री ने कहा -‘हजरत,क्या मुजाइका है ? रास्ते में बातों से जी बहलता है।’
मीर साहब बिगडक़र बोले-‘जी, आपका तो जी बहलता है, मगर मेरी जबान खराब होती है।’
देश फिलवक्त सुप्रीम कोर्ट बनाम केन्द्र सरकार की ऊहापोह को दिलचस्पी के साथ देखता हुआ भौंचक भी है। यह मुद्दा आम आदमी की समझ, पहुंच या बहस के इलाके का नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तथा राज्यों के हाई कोर्ट फिलवक्त जूझ रहे हैं कि उनके यहां स्वीकृत संख्या मेंं जज नहीं हैं तो न्याय कैसे करें। सरकारी तेवर मेंं इतनी हेकड़बाजी है कि वह जजों की नियुक्ति को लेकर अपना दखल तो चाहती ही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह मामला उनके इलाके का है और सरकार का हस्तक्षेप इसमें नहीं चाहिए।
एक पुराना किस्सा है। एक गुरुजी के दो शिष्य थे। दोनों में पटती नहीं थी। तो सोने जाने के पहले गुरुजी ने दोनों को अलग अलग कर कहा कि तुम लोग मेरा एक एक पैर दबाओ और मैं सोता हूं। इसमें एक दूसरे से लडऩे की जरूरत नहीं है। गुरुजी खर्राटे लेने लगे। नींद में अचानक उनका एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ गया। जिस शिष्य के हिस्से का पैर नीचे दबा था, उसने गुरुजी के आक्रमणकारी पैर पर लाठियां दे मारीं। बुरी तरह चोटिल होकर गुरुजी उठे। तब उन्हें मालूम हुआ कि माजरा क्या है। दोनों को अलग अलग रहने की हिदायत देकर कितनी बड़ी भूल हो गई! हर हालत में गुरुजी को हिदायत देने के बाद सोना नहीं था। यही हाल भारतीय संविधान नामक गुरुजी के पिछले 70 बरस से सोए रहने के कारण हुआ है। सवाल है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन सा षिष्य करेगा। सुप्रीम कोर्ट या केन्द्र सरकार?
संविधान सभा में इस पर बहस हुई। सबसे बेहतर, तर्क वैज्ञानिक और भविष्यमूलक तकरीर प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर की थी। उस पर ही संविधान सभा के सदस्यों की समर्थन की मुहर लगी। अम्बेडकर ने कहा था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को भारत के चीफ जस्टिस की सहमति से नियुक्त करने का सवाल भी पेचीदा है। उस पर बहुत वस्तुपरक और तटस्थ लेकिन नागरिक हितों को ध्यान में रखकर विचार करना होगा। यह भी सुझाव है कि जजों की नियुक्ति का समर्थन संसद के दो तिहाई बहुमत से हो। तीसरे यह भी कि उनकी नियुक्ति के लिए राज्यों का समर्थन लिया जाए। तरह तरह की सलाहों के दलदल में अम्बेडकर को वह सर्वमान्य और भविष्यमूलक रास्ता ढंूढऩा पड़ा जो भारत के संविधान का आज हिस्सा है। उन्होंने कहा ग्रेट ब्रिटेन में ऐसे जजों की नियुक्ति सम्राट करता है, अर्थात उसे कार्यपालिका को करना होता है। इसका ठीक उलटा अमेरिका में है। वहां ऐसे जजों की नियुक्ति अमेरिकी सीनेट की सहमति सेे होती है। उन्होंने कहा कि भारत जिस तरह के हालात में है, वहां ये दोनों रास्ते हमारे लिए मुफीद नहीं हैं। हमारे जनप्रतिनिधि इन देषों के मुकाबले राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व नहीं हैं। ऐसी हालत में केवल कार्यपालिका या संसद या राज्यों की विधानसभाओं पर नियुक्ति का यह अधिकार छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे में राजनीतिक दबाव और राजनीतिक प्राथमिकताएं सिर चढक़र बोलेंगी। हमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। हो सकता है वह रास्ता कठिन या पेचीदा हो। जजों की नियुक्ति के मामले में हम राष्ट्रपति अर्थात कार्यपालिका को सभी अधिकार नहीं सौंप सकते। उसके लिए विधायिका के समर्थन की भी जरूरत नहीं है। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति की सलाह लेना जरूरी है जो न्याय के इलाके का विषेषज्ञ हो और राष्ट्रपति अर्थात केन्द्र सरकार को सही और मुनासिब सलाह दे सके।
अम्बेडकर ने कहा जो लोग नियुक्ति का पूरा दारोमदार चीफ जस्टिस पर सौंपना चाहते हैं। वे समझते होंगे कि चीफ जस्टिस बहुत काबिल होने के साथ साथ निष्पक्ष भी होंगे। मैं भी यही मानता हूं, लेकिन आखिकार चीफ जस्टिस भी एक मनुष्य ही तो हैं। उनमें भी एक साधारण व्यक्ति की तरह पूर्वग्रह, पसंदगी, नापसंदगी और आंकलन करने की ताकत में कोई दोष भी हो सकते हैं। इसलिए नियुक्ति के मामले में चीफ जस्टिस सरकार के फैसले पर वीटो कर दें। यह भी ठीक नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला एक अरसे से ढुलमुल विवादग्रस्तता में पनाह पाता कराहता रहा है। नए लोकतंत्र में प्रधानमंत्री नेहरू भारत के चीफ जस्टिस से टेलीफोन पर बतिया लेते और नियुक्ति हो जाती थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 7 थी। अब बढक़र 25 हो गई है। अब नेहरू भी नहीं हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस अपने पूर्वजों का उत्तराधिकारी संस्करण भी नहीं हैं। पदेन भले हों। अब हर बात के लिए क्यों कहा जाता है कि इस गिरावट के लिए नेहरू जिम्मेदार हैं।
घिसटता घिसटता यह मामला आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ही हल किया। सुप्रीम कोर्ट के लिए अक्टूबर का महीना संयोगों वाला है। 26 अक्टूबर 1990 को सुभाष षर्मा बनाम भारत संघ के मामले में जजों ने पाया कि कोर्ट का एक पुराना फैसला एस. पी. गुप्ता के मामले में 1981 में दिया गया था। उस पर दुबारा विचार की जरूरत थी क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता, मर्यादा और विषेषज्ञता को दरकिनार कर सरकार को साहबे आलम कहता पक्षपात करता है। एस. पी. गुप्ता के मामले में जस्टिस पी. एन. भगवती ने फजल अली, डी. ए. देसाई और वेंकटरमैया की भी तरफ से फतवा दे दिया था कि जजों की नियुक्ति के मामले में भारत के चीफ जस्टिस की वरीयता या प्राथमिकता नहीं है। वह तो केन्द्र सरकार की है। उसे ही सभी संवैधानिक अधिकारियों से सलाह कर जजों का चयन करना है। उन्होंने यह भी लिखा कि भारत के चीफ जस्टिस की सलाह से चलना या उसे मानना केन्द्र सरकार के लिए बंधनकारक नहीं है। केन्द्र सरकार चाहे तो जजों की नियुक्ति के लिए नाम भी दे सकती है। भले ही संविधान की मंषा हो कि यह षुरुआत भारत के चीफ जस्टिस को करनी है।
फिर यह मामला 1993 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने हल किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 (2) में लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीष की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायाधीष से सदैव परामर्ष किया जाएगा। परामर्ष शब्द का तकनीकी अर्थ है केवल सलाह या राय लेना। उसे दरकिनार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को यह व्याख्या गंवारा नहीं हुई, जो उनके पूर्वज जजों ने तय कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसकी सलाह प्राथमिक होगी। यह सवाल तब उठेगा जब संबंधित संवैधानिक पदाधिकारियों में मतभेद हो जाए। आपस में सलाह करना बिल्कुल जरूरी है लेकिन किसकी सलाह मानी जाए? इसके लिए कौन विशेषज्ञ हैं? इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। जिन संभावित जजों से काम लेना है और जो वकील या जज अब तक काम करते आए हैं। उनकी लियाकत और गुणवत्ता तथा न्याय दृष्टि का सही आंकलन तो आखिरकार भारत के चीफ जस्टिस को ही करना होता है। केन्द्रीय मंत्रिपरिषद या अन्य संवैधानिक अधिकारियों को नहीं। इसलिए परामर्श का अर्थ केवल मुंह छू लेना नहीं है। चीफ जस्टिस की राय को अहमियत देनी होगी क्योंकि वे फकत चीफ जस्टिस नहीं हैं। न्यायिक प्रकिया के सबसे वरिष्ठ और उच्चतर विशेषज्ञ हैं। उनका राजनीतिक प्रभावों या दबावों से कुछ लेना-देना नहीं है। इसलिए परामर्श शब्द को सहमति के अर्थ में लिया जाए। अन्यथा जजों की नियुक्ति में वायरस आ सकता है।
अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केन्द्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू सरकार की श्रेष्ठता पर टिप्पणियां कर रहे हैं। इन दोनों संवैधानिक पदाधिकारियों की बौद्धिक क्षमता जजों, वकीलों और कानूनविदों की आड़ में आला दर्जे की नहीं है। धनखड़ यह भी कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को विधायिका के फैसलों को बातिल करने का अधिकार नहीं है। यह पूूरे संवैधानिक ढांचे और उसके फलसफा की ही हेठी करता है।
किरण रिजिजू का यह सवाल कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधि भी होने चाहिए। खुद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 सदस्यों की पीठ ने पहले ही खारिज कर दिया है। उनका यह कथन भी बेतुुका है कि जज जनता द्वारा चुने नहीं जाते। इसलिए उन्हें जनता के प्रतिनिधियों से कमतर भूमिका देनी चाहिए। यह तो संविधान के ढांचे का एक तरह से अपमान हुआ। हर वह व्यक्ति सबसे बड़ा देषभक्त या जनसेवक नहीं हो सकता, जो केवल चुनाव जीतकर आए।
इसलिए एडवोकेट ऑन रेकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा दायर मामले में अक्टूबर 1993 में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की अहमियत को बरकरार रखते हुए भी उसमें प्रजातांत्रिकता का पुट देने की कोशिश की। कोर्ट ने कॉलेजियम नाम के एक नए फेनोमेना या उपग्रह का आविष्कार किया और कहा कि चीफ जस्टिस के बदले सुप्रीम कोर्ट के बाद पांच वरिष्ठ जजों के सामूहिक विवेक को चीफ जस्टिस पढ़ा जाए। फिर उनसे परामर्ष को उनकी सहमति का दर्जा दिया जाए, उससे कमतर कुछ नहीं। यही प्रक्रिया चल रही है।
2014 में सरकार की एक और कोशिश नाकाम हुई। जब सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2015 में केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को खारिज कर दिया। उसमें भी जनप्रतिनिधियों को प्राथमिकता बल्कि बहुमत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के साथ संबद्ध कर सुप्रीम कोर्ट की अहमियत को कमतर करने की कोशिश की गई थी। मनोनीत नौकरषाहों और अल्प अवधि के लिए चुने गए मंत्रियों को रख देने से भी कौन सी न्यायिक क्रांति हो जाती? उनमें से कई अकादमिक नजरिए से बेहद जहीन भी नहीं कहे जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का रिकार्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। ए. डी. एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला के मामले में जब इंदिरा गांधी द्वारा लाए गए आपातकाल को चुनौती का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। तब संविधान पीठ के 5 में से 4 जज इस कदर आपातकाल के पक्ष में हो गए कि कहा कि आपातकाल में नागरिकों के संवैधानिक अधिकार सरकार द्वारा छीने जा सकते हैं। उनमें एक जज यशवंत चंद्रचूड भी थे जिनके पुत्र धनंजय चंद्रचूड़ अभी भारत के चीफ जस्टिस हैं। अपने पिता द्वारा निर्धारित संवैधानिक व्यवस्था को तार तार करते मौजूदा चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने पुट्टास्वामी के नए मामले में नौ जजों की बेंच की ओर से निजता और नागरिक आजादी के संवैधानिक अधिकारों को फिर से बहाल किया है। उन पिछले चार जजों ने आपातकाल हटने के बाद बारी-बारी से कहीं न कहीं एक तरह से माफीनामा देते हुए कहा था कि वे आपातकाल के वक्त डर गए थे। एस. पी. गुप्ता के मामले में बहुमत ने फिर सरकार के पक्ष में फैसला किया। तब फिर 1981 में इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थीं। 2015 का फैसला राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम को ध्वस्त करता हुआ जब हुआ, तब तो मोदी सरकार थी। जब तक 11 सदस्यीय बेंच नहीं बन जाए। तब तक सुप्रीम कोर्ट के 1993 और 2015 के फैसलों के खिलाफ कानून मंत्री के उलाहने और उपराष्ट्रपति के आलिम फाजिल बनने के पोज से क्या कुछ होने वाला है।
पिटना तो जनता को है। कॉलेजियम प्रणाली के जरिए जजों के बाल बच्चे तो फलफूल रहे हैं। सबसे बुरी हालत हाई कोर्ट में है। वहीं प्रैक्टिस करते करते वे भाई बहन, बेटे बेटी और अन्य निकट रिश्तेदार जज बना दिए जाते हैं जिनके सबसे निकट के रिश्तेदार उसी हाई कोर्ट में जज होते हैं। अपने उत्तराधिकारियों का चुनाव करने में दखल देते हैं। चाहे कॉलेजियम हो या मंत्रिपरिषद हो। यदि जज और मंत्री के चरित्र में खोट आ जाए तो भोगना तो जनता को है। यह बात भी बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में ठोक बजाकर कही थी।
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
स्वर्गीय मुलायमसिंह यादव को पद्मविभूषण सम्मान क्या मिला, देश में बहस छिड़ गई है। सबसे पहले तो सबको आश्चर्य यह हुआ कि मुलायम को यह सम्मान उस भाजपा की सरकार ने दिया है, जिसे देश में सबसे ज्यादा यदि किसी ने तंग किया है तो उ.प्र. के मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव ने किया है। राम मंदिर के लिए हुए प्रदर्शनों में भाजपा नेताओं और कार्यकर्त्ताओं की जैसी धुनाई मुलायम ने की, क्या किसी और मुख्यमंत्री ने की?
शंकराचार्य को गिरफ्तार करने की हिम्मत क्या आज तक किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की हुई? यदि मुलायमसिंह का स्वास्थ्य उनका साथ देता तो वे ही ऐसे एक मात्र नेता थे, जो नरेंद्र मोदी की हवा खिसका सकते थे। उनके प्रशंसक सारे देश में मौजूद थे लेकिन वे इतने दरियादिल भी थे कि संसद में उन्होंने खुले-आम मोदी की प्रशंसा भी की लेकिन क्या इसीलिए मुलायम को भाजपा ने पुरस्कृत कर दिया है? शायद नहीं। यदि मोदी पर किए गए अहसानों का सवाल है तो ऐसे दो-चार लोग तो अभी भी जिंदा हैं, जिन्हें भारत रत्न भी दिया जाए तो वह भी कम ही रहेगा। तो मुलायम को क्यों दिया गया है, यह सम्मान?
मेरी राय में यह सम्मान नहीं है। यह सरकारी रेवड़ी है, जो मरणोपरांत और जीते-जी भी बांटी जाती है। गरीब जनता को बांटी गई रेवडिय़ां और इस तरह के सम्मानों की रेवडिय़ों में ज्यादा फर्क नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस रेवड़ी को अपना रेवड़ा बनाकर सबसे पहले इसे खुद के हवाले कर लिया था। अब मुलायमजी को दी गई इस रेवड़ी की उन्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। यदि वे जिंदा होते तो वे कह देते कि उन्होंने मीठा खाना छोड़ दिया है।
अभी तक जितने लोगों को भारतरत्न मिला है, उनमें से दो-तीन लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर से खूब जानता रहा हूं। वे लोग भाई मुलायमसिंह के पासंग के बराबर भी नहीं थे। इसीलिए समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का यह कथन थोड़ा बेहतर है कि अगर मोदीजी ने मुलायम को कुछ देना ही था तो भारत रत्न ही देना था। इन समाजवादियों को लग रहा है कि यह मुलायमजी का सम्मान नहीं, उप्र के यादव वोटों को बटोरने का पैंतरा है।
यदि अखिलेश या उनकी पत्नी यह सम्मान लेने पहुंच गई तो भाजपा की यह रेवड़ी उसका रसगुल्ला बने बिना नहीं रहेगी। अखिलेश के लिए भाजपा ने यह बड़ी दुविधा पैदा कर दी है। भाजपा के कुछ नेताओं को ऐसा भी लग रहा है कि यदि मुलायमसिंह को वे अपना बना लें तो अखिलेश को हाशिए में सरकाना उनके बाएं हाथ का खेल होगा। उनकी एक रणनीति यह भी हो सकती है कि अगले चुनाव में भाजपा और सपा का गठबंधन बन जाए। जहां तक अखिलेश का सवाल है, उसे डॉ. लोहिया के समाजवादी सिद्धांतों का कोई खास आग्रह भी नहीं है और जानकारी भी नहीं है। इसीलिए भाजपा के साथ गठबंधन करने में सपा को ज्यादा कठिनाई भी नहीं होगी। यह सम्मान गजब का पैंतरा भी सिद्ध हो सकता है। (नया इंडिया की अनुमति से)
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
हर साल 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस बड़े जोर-शोर से मनाते हैं। राष्ट्रपति भवन के सामने इंडिया गेट या अब कर्तव्य पथ पर हम अपनी फौजी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। राष्ट्रपति भवन में विशाल प्रीति-भोज का आयोजन भी होता है। यहां सवाल यह उठता है कि क्या गणतंत्र दिवस को मनाने का यही सर्वश्रेष्ठ तरीका है? गणतंत्र दिवस का यदि कोई दूसरा सरल नाम हम बोलना चाहें तो उसे संविधान प्रवर्तन दिवस भी कह सकते हैं।
इसी दिन हमारा संविधान अब से 73 साल पहले लागू हुआ था। इसी दिन भारतीय गणतंत्र की शुरुआत हुई थी। इस दिन भारत की फौजी ताकत का प्रदर्शन क्या हमारे संविधान को कोई शक्ति प्रदान करता है? फौजी ताकत तो सोवियत संघ और साम्यवादी चीन के पास हम से भी कहीं ज्यादा रही है लेकिन क्या हम उन्हें कभी गणतंत्र कहते थे? वे तो पार्टीतंत्र रहे हैं। नेतातंत्र रहे हैं। तानाशाह राष्ट्र रहे हैं। हमने भी आजाद भारत में सोवियत संघ की नकल शुरु कर दी। वहां हिटलर और मुसोलिनी को पराजित करनेवाली सेना का हर साल प्रदर्शन किया जाता था।
हमने भी वही शुरु कर दिया लेकिन उसके लिए दिन ऐसा चुन लिया, जिसका गणतंत्र या लोकतंत्र से कुछ लेना-देना नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत की सैन्य-शक्ति का प्रदर्शन अनुचित है लेकिन एक उत्तम गणतंत्र दिवस के दिन भारत की लोकशक्ति का स्मरण, प्रदर्शन और संवर्धन करना ज्यादा जरुरी है। 26 जनवरी का दिन बस एक शासकीय दिन बनकर रह जाता है। लोग घर बैठकर छुट्टी मनाते हैं। इस दिन यदि देश और प्रदेश की सरकारें हमारे गणतंत्र को मजबूत और स्वस्थ बनाने के नए-नए संकल्प करें तो सचमुच हम अपना गणतंत्र दिवस सही अर्थों में मना सकते हैं।
क्या हमने कभी सोचा कि भारत का राज-काज हम पूरी तरह से गणभाषा या लोकभाषा में चला पाए हैं? क्या हमने हमारी अदालतों की दुर्दशा पर इस दिन कोई विचार किया? चार करोड़ से ज्यादा मुकदमे दशकों से हमारी अदालतों में लटके पड़े हुए हैं। भारत में शिक्षा और चिकित्सा की तरह न्याय भी दुर्लभ है। हमारे अयोग्य, भ्रष्ट और निकम्मे जन-प्रतिनिधियों को वापस बुला लेने की विधियां अभी तक क्यों नहीं बनी हैं? जनता निहत्थी होकर पांच साल तक इंतजार क्यों करे?
आज तक भारत में एक भी सरकार ऐसी नहीं बनी है, जिसे कुल वयस्कों के 50 प्रतिशत वोट भी मिल सके हों। कुल मतदाताओं में से 20-30 प्रतिशत लोगों के वोट से बनी सरकारें अपने आप को पूरे देश का प्रतिनिधि बताती हैं। हमारे राजनीतिक दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में तब्दील हो चुके हैं। उनका आंतरिक गणतंत्र या लोकतंत्र एक मुहावरा बनकर रह गया है?
सारे सांसदों, विधायकों और सरकारी अफसरों की चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा हर गणतंत्र दिवस पर सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता ताकि भ्रष्टाचार पर थोड़ी-बहुत लगाम तो लगे। हमारा संविधान अभी तक कायम है, 100 से ऊपर संशोधनों के बावजूद, यही हमारी बड़ी उपलब्धि जरुर है।
(नया इंडिया की अनुमति से)
-कनक तिवारी
बुद्धिपुत्रों को आत्मश्लाघा के दलदल में डालना एक कुत्सित सरकारी षड्यंत्र है। इस संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय की निर्देशावली भी पब्लिक ऑडिट मांगती है। संविधान के अनुच्छेद 18(1) में लिखा है" राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा"। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान के मूल अंग्रेजी पाठ का हिंदी मानक पाठ विद्या संबंधी किया गया है जबकि वह अंग्रेजी में यह कहता है" No title not being a military or academic distinction shall be conferred by the State".। कोई बताए कि अंग्रेजी शब्द डिस्टिंक्शन का हिंदी अनुवाद विद्या संबंधी कैसे हो गया ? उसे तो प्रावीण्य होना चाहिए था। अर्थात अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन और हिंदी में बिना प्रावीण्य पद्म पुरस्कार दिए जा सकते हैं।
पद्म पुरस्कारों का एक सरकारी तिलिस्म और है । इन्हें सरकारी नौकरी की तरह पदोन्नति की सीढ़ियां बना दिया गया है । आज पद्मश्री कल पद्मभूषण परसों पद्म विभूषण । अपने जीवन की बौद्धिक सामाजिक उपलब्धि के कारण यदि कोई पद्मश्री के ही काबिल है। तो वह कुछ वर्षों में पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण होने के लायक प्रोन्नत कैसे हो जाता है। क्या वह अचानक श्रेष्ठ होकर पांच 10 वर्षों में ज्यादा योग्य हो जाता है।
देश के सबसे बुजुर्ग और गांधीवाद के लगभग शीर्ष अध्येता डॉक्टर रामजी सिंह को 93 वर्ष की उम्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया । 91 वर्ष के सच्चिदानंद सिन्हा जैसे श्रेष्ठ समाजवादी गांधीवादी ऋषि चिंतक को आज तक सरकार ने अन्य किसी सम्मान के लायक समझा ही नहीं। ऐसे कई समाज विचारक हैं। उनके नाम से सत्ता प्रतिष्ठान की घिग्गी क्यों बंध जाती है? संस्कृति के श्रेष्ठ विद्वान गोविंद चंद्र पांडेय को कुछ वर्ष पहले पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। उसी वर्ष हिंदी के एक चुटकुलेबाज हंसोड़ कवि कहलाते व्यक्ति को यही सम्मान दिया गया था। देशद्रोह के आरोप से आरोपित व्यक्ति को भी पहले पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाने की शिकायतें मिली हैं। सरकारी फाइलों में अपने नाम चुपके चुपके सरकारी अधिकारी या उनके मददगार चिपकाते रहते हैं। जैसे चूहे फाइलें चुपके-चुपके ही उतरते रहते हैं । इस संबंध में जनता के सामने पारदर्शी ढंग से सरकार कभी कोई विचार नहीं करती क्योंकि उसे खतरा होता है कि उसके गलत काम शायद पकड़ लिए जाएंगे । हालांकि सरकारें सब काम गलत नहीं करती हैं।
यदि पद्म सम्मान की प्राथमिक सूचियों को देखा जाए तो उनमें सबसे ज्यादा नाम सरकारी अधिकारियों या उनसे जुड़े हुए लोगों के ही होते हैं। सरकारी संपत्ति, सूचनाओं, संपर्कों, योजनाओं वगैरह के आधार पर जो रचनात्मक कार्य किए भी जाते हैं। उनके लिए समाजचेता सम्मानों की योग्यता या वांछनीयता कैसे बन सकती है? सुना है पद्म सम्मान के लिए आवेदन पत्र भी मंगाए जाते हैं । यदि ऐसा है तब तो उसके कई ठनगन भी होंगे । यह तो शायद अच्छा ही होगा कि आवेदन पत्रों के साथ शपथ पत्र नहीं मंगाए जाते होंगे ।अन्यथा झूठी सूचनाओं का दोषी पाकर फौजदारी मुकदमा भी चलाया जा सकता है। कोई नहीं जानता कि जूरी या निर्णायक मंडल में किसे रखा जाता है और किन आधारों पर । यह तो लोकतांत्रिक उत्कृष्टता का तकाजा है कि यह बात पारदर्शी ढंग से जनता को मालूम होनी चाहिए।
सरकारी सम्मानों का एक अर्थ यह भी है कि किसी की पीठ पर छुरे मारे जाते हैं और किसी की पीठ थपथपाई जाती है। अखबारों में वैवाहिक विज्ञापन प्रकाशित होते रहते हैं। उसमें विवाह के लिए युवक युवतियों के ऐसे फोटो और विवरण छपते हैं। जो सही नहीं होते। खुद का प्रतिष्ठित कारोबार के नाम से देशी दारू के गद्दीदार विज्ञापित होते हैं। सुगठित डीलडौल वाले मधुमेह उच्च रक्तचाप वगैरह के मरीज होते हैं। घर के सभी कार्यों में दक्ष सुलक्षणा चाय तक बनाने में रुचि नहीं रखती। क्या लेखकों कलाकारों बुद्धिजीवियों संस्कृति कर्मियों और समाज सेवकों से इसी तरह की जानकारी या आवेदन सरकार मांगना चाहती होगी? कई इलाकों में सम्मान देने की फूहड़ परंपराएं इस देश में हैं। खेल रत्न या अर्जुन पुरस्कार पाने के लिए अच्छे खिलाड़ियों को भी अपना बायोडाटा लेकर मंत्रियों के दरवाजों पर उनकी ड्यौढि़यों पर खड़े रहना पड़ता है।
कोई भी सरकार अपने विपक्षी नेताओं को विद्यार्थियों को और श्रमिकों की यूनियनों के नेताओं को पद्म सम्मान उसे नवाजना उचित नहीं समझती। पद्म सम्मान मिल जाने का खतरा उनके लिए भी बढ़ता जा रहा है जो कतई लेखक या संस्कृति कर्मी नहीं है लेकिन सरकारी फाइलों में इसी योनि में पैदा कर दिए जाते हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दो प्रकरणों में पद्मश्री को अपनी उपाधि की तरह लिखने वाले सज्जनों के खिलाफ आदेश दिया था कि यह बंद हो। नहीं तो उनकी पद्मश्री की सम्मान वाली उपाधि वापस ले ली जाए। कई है जिनके लेटर हेड पर विजिटिंग कार्ड पर पद सम्मान का ठसका अंकित रहता है। जिस तरह खलवाट में बाल ढूंढे जाते हैं वैसे ही सरकार कई नए साहित्य परिवार अन्वेषित करती रहती हैं। हर लेखक बड़ा नहीं हो सकता । बड़ा होना ही पुरस्कार पाने का पैमाना नहीं है। लेकिन बड़े पुरस्कार पाने का पैमाना जरूर बन गया है।
केंद्रीय सरकार के कार्यालय साहित्य संस्कृति कला विद्वता समाज सेवा के मीना बाजार कांजी हाउस या रोजगार कार्यालय नहीं है, जहां पंजीयन कराया जाए ।लाइसेंस लिया जाए या मनुष्य की प्रतिभा की फौती पैदाइश का प्रमाण पत्र जारी कराया जाए।
-स्मिता
काष्ठ शिल्प के सिद्धहस्त कलाकार, पर्यावरणविद और समाज सुधारक, और इस बरस पद्मश्री से सम्मानित अजय मंडावी कांकेर जिले का गौरव हैं। आदिवासी समुदाय के इस कलाकार की अद्भुत कला और शिल्प से पूरे प्रदेश को नई पहचान मिली है।
एक साधारण आदिवासी गोंड़ परिवार में जन्में मंडावी का रूझान बचपन से ही कला की ओर रहा । गांव में नदी किनारे छोटे छोटे नाव बनाने, गणपति की मूर्ति बनाने से उनकी कला यात्रा की शुरूआत हुई। आने वाले वाले वर्षो में अपने जुनून और प्रतिभा के बल पर उन्होने असंभव दिखने वाले कई कार्यो को मूर्त-रूप दिया।
किसी भी प्रकार के विधिवत प्रशिक्षण और किसी तरह की आर्थिक सहायता के बिना, अपने ही सीमित संसाधनों से उन्होंने कला के क्षेत्र में जिन ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है, वह आने वाली पीढ़ी के लिये निश्चित ही प्रेरणास्पद है।
अजय मंडावी के विरले व्यक्तित्व और अनूठी कला की प्रेरणा, कांकेर के स्थानीय विद्यार्थियों के साथ-साथ जेल में कैद, बंदियों के जीवन की दिशा को सृजनात्मक तरीके से बदलने में भी कारगर सिद्ध हुई। इसी प्रेरणा के सहारे अजय मंडावी ने सीमित संसाधनों के साथ अपने असीमित स्वप्नों को साकार करने की उड़ान भरी। उनकी प्रेरणा से आज लगभग 400 युवाओं ने अपराध और हिंसा का रास्ता छोड़कर शिल्पकला को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। इस लिहाज से यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि अजय मंडावी, व्यक्तिगत रूप से सैकड़ों कैदियों का पुर्नवास करने वाले देश की इकलौती शख्सियत हैं। इनमें बहुत से माओवादी विचारों से प्रभावित कैदी भी शामल है।
अजय मंडावी जैसे सिद्धहस्त गुरु के सान्निध्य में छैनी-हथौड़ी से एक लकड़ी के टुकड़े पर अक्षर उकेरते हुए बंदियों को प्रत्यक्ष देखकर ऐसा प्रतीत होता है, मानो ये बंदी अपने भीतर की हिंसात्मक मनोवृतियों को भी काट-छांट कर अपने जीवन को सृजनात्मक स्वरूप प्रदान कर रहे है। जब कोई भी कला या शिल्प, एक हिंसक अपराधी के मन-मस्तिष्क को कायांतरित करके संवेदनशील मनुष्य और फिर उससे भी आगे एक बेहतरीन कलाकार बना दे, तो यहीं पर आकर कला अपने उच्चतम शिखर को प्राप्त कर लेती है, जिसे अजय मंडावी ने अकेले ही संभव कर दिखाया है।
अपनी कला की यात्रा में अजय मंडावी ने अनेक सुंदर प्रतिमानों को गढ़ा, और बहुत सी वर्जनाओं को तोड़ा भी । उनकी कला यात्रा में गोल्डन बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड, लिम्का बुक आफ रिकार्ड सहित कामयाबी और शोहरत के बहुत से चमकीले और यादगार मुकाम आते रहे हैं।
लेकिन वे खुद अपना योगदान उसी प्रयास को मानते है, जिसमें कला के माध्यम से कोई भटका हुआ आदिवासी युवा अपराध और हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा मे शामिल हो जाता है । उनकी आत्मा की यही सुवास, मद्धिम मुस्कान के साथ उनके चेहरे और जीवन में सहज रूप से परिलक्षित होती है ।
शानदार व्यक्तित्व के धनी और काष्ठशिल्पकार अजय मंडावी कई सौ युवाओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में "गुरूजी" के नाम से जाने जाते है । बकौल अजय मंडावी कोई भी कला, अपने सामाजिक सरोकरों से न्याय करते हुए जब व्यापक स्वीकार्यता के उजले धरातल पर गहरी जड़ें जमा लेती है, तभी वह अपने सर्वश्रेष्ठ रूप-सौदर्य के साथ उच्चतम स्तर पर प्रकट हो पाती है।
अजय मंडावी जैसे कलाकार पहली नजर में बेशक एक आम मनुष्य की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन अपने जुनून, निष्ठा, मेहनत, प्रतिभा और गहरी अंतर्दृष्टि के साथ कला के माध्यम से उन्होंने सामाजिक विकास में जो योगदान दिया है, वह निश्चित ही उन्हें असाधारण बना देता है। उनकी कला यात्रा के प्रारंभिक साक्षी उनका परिवार, आदिवासी समाज, बंदियो का समूह, पुलिस प्रशासन सहित स्थानीय प्रशासन रहे हैं, किन्तु समय के साथ उनकी कला को देश के कोने-कोने और दुनिया के अनेक देशों में भी प्रतिष्ठा मिल चुकी है ।
उनकी कला शिल्प का मुख्य उद्देश्य समाज के भटके हुए (विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र के) लोगों का शिल्पकला के माध्यम से सर्वांगीण विकास करना ही रहा है । साथ ही इन स्थानीय लोगों के सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक तथा शैक्षणिक स्तर में बढ़ोत्तरी करते हुए इन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में भी वे सफल रहे हैं।
अजय मंडावी के प्रमुख योगदान को हम इन सोपानों में देख सकते है:-
1 वंदे मातरम
18 जनवरी 2018 का दिन कांकेर जेल के लिए एक ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज हुआ। यह अवसर जेल में कैद बिंदियों का हिंसा और आपराधिक माहौल से इतर सांस्कृतिक पक्ष का एक सशक्त हस्ताक्षर करने का था। कांकेर का जिला जेल, पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला जेल है जिसके नाम से गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
"अबकी बार लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा "- कुंवर नारायण
बिल्कुल इसी तर्ज पर अजय मंडावी के मार्गदर्शन में कुल नौ बंदियों ने दिन-रात मेहनत करते हुए 20 फीट चौड़ा, 40 फीट लंबी लकड़ी की तख्ती पर वन्दे मातरम राष्ट्रीय गीत को काष्ठशिल्प के रूप में उकेर दिया ।
18 तारीख की सुबह अपनी नई किरण, नये उजास लेकर आया,जब कंकर जेल के ही 40 कंबलों के उपर अजय मंडावी की टीम ने अपनी कला का प्रदर्शन किया । इस शिल्प को ऐतिहासिक अनुकृति (कल्ट) का दर्जा देते हुए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड से नवाजा गया।
2- शांता आर्टस स्वयं सहायता समूह
मुख्यतः शांता आर्टस कला समूह, ऐसे बंदी समूह का प्रतिष्ठित नाम है, जिसके अधिकांश सदस्य, अलग अलग समय में नक्सली वारदात से छूटकर कला के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में जुड़ गये थे। यह एक ऐसा सेतु है, जो कैदियों के पुनर्वास के लिए, नैतिक विधि से आर्थिक उपार्जन करने के लिए बनाया गया है। इसके प्रशिक्षक और मार्गदर्शक अजय मंडावी रहे, जो कैदियों को कला की शिक्षा देने के साथ ही, उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से भी समाज में एक बेहतर मनुष्य के रूप में गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार करते हैं ।इतना ही नहीं, वे इन कैदियों को बेहतर सामाजिक वातावरण भी रचते हैं।
-संजय श्रमण
अमत्र्य सेन अपनी प्रसिद्ध कृति ‘द आग्र्यूमेंटेटिव इंडियन’ में दो महत्वपूर्ण धारणाओं के प्रति सावधान करते हैं। उनके अनुसार हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि लोकतंत्र पश्चिम द्वारा दिया गया एक उपहार है जिसे भारत ने आजादी के तुरंत बाद सीधे सीधे अपना लिया है।
वे एक दूसरी धारणा को भी निशाने पर लेते हैं। वह दूसरी धारणा यह है कि भारत अतीत में कभी लोकतान्त्रिक था। अक्सर भारत का महिमा गान करने वाले लोग कहते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसा कुछ विशेष है जो भारत को लोकतंत्र के अनुकूल बनाता है। सेन इस दूसरी धारणा को भी बहुत हद तक नकारते हैं।
अमर्त्य सेन द्वारा कही गई इन दो बातों के बहुत गहरे निहितार्थ हैं। इन दो बिंदुओं को ध्यान से देखिए।
वह लोकतंत्र, जिसे आज हम देखते हैं या हासिल करना चाहते हैं, उसका प्राचीन भारत या किसी भी देश में कोई उदाहरण नहीं मिलता। जो उदाहरण प्राचीन साहित्य में उपलब्ध हैं वे लोकतंत्र की धारणा के कुछ निकट आते हैं, वे लोकतंत्र के कुछ आदिम रूपों का इशारा भर देते हैं।
लेकिन यह कह देना कि भारत या कोई अन्य सभ्यता में लोकतंत्र था- यह एक षड्यंत्र है। प्राचीन भारत में हम लोकतान्त्रिक थे, यह कहकर असल में एक खास किस्म की ‘प्राचीन यशगाथा’ को बिना सबूतों के दोहराने की भक्त मानसिकता मजबूत की जाती है। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि आधुनिक लोकतंत्र ही नहीं किसी भी तरह का शुभ या सद्गुण किसी एक सभ्यता या समाज के द्वारा दूसरी सभ्यता या समाज को दान में नहीं दिया जा सकता।
अब भारत और भारतीयों की दिक्कत यह है कि एक खास तबका उस प्राचीन यशगाथा को बहुत ही रूमानी बनाकर पेश करता है। वह तबका दुनिया का सारा विकास और शुभ अपने उस सतयुग में ठूँसकर दिखाना चाहता है। वह भी इसलिए ताकि देश और समाज को वास्तविक रूप से सभ्य होने की मेहनत किये बिना सभ्यता का सर्टिफिकेट मिल जाए और फिर उनका जो जी में आए वे इस देश में कर सकें। ये भारतीय सत्ताधीशों की ही नहीं दुनिया के सभी समाजों के धर्म-सत्ता और राजसत्ता के अधिपतियों की पसंदीदा रणनीति रही है।
इस रणनीति के तहत यह कहा जाता है कि सारा शुभ अतीत में कहीं था जो समय की लहर में कहीं बह गया है इसलिए हमें भविष्य में नहीं बल्कि अपने ‘वास्तविक अतीत’ में जाकर खुदाई करनी चाहिए।
यह खतरनाक रणनीति इतनी सफल रहती आई है कि पूरे देश का जनमानस इसके जाल में तुरंत फस जाता है। प्राचीन स्वर्णयुगों की तस्वीर दिखाकर भविष्य के सपने बुनना और इन सपनों के लिए कुर्बानी मांगना– यह सभी देशों और समाजों के तानाशाहों का पसंदीदा खेल रहा है। भारत इस अर्थ मे विशेष रूप से बदनसीब है क्योंकि यहाँ यह खेल राजनीति या सत्ता तक सीमित नहीं है।
गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि भारत में यह खेल भारत के सबसे बड़े और प्रचलित धर्म और अध्यात्म का भी मूल नियम बन चुका है। इसीलिए डॉ अंबेडकर ने इसे धर्म नहीं राजनीति कहा था।
यह षडय़ंत्रकारी तबका यह कहता है कि समाज का सुख ही नहीं बल्कि व्यक्ति का मोक्ष भी अतीत के स्वर्णयुग या सतयुग में कहीं पीछे छूट गया है। समाज का स्वर्णकाल ही नहीं बल्कि व्यक्ति का निर्वाण भी अतीत के किसी गड्ढे में गिरा पड़ा है। ये दोनों धारणाएं एकसाथ भारत के लोकमानस को परोसी जाती हैं।
इसलिए ताज्जुब नहीं कि जिन लोगों ने भारत के सतयुग को भारत का भविष्य बनाने का प्रोजेक्ट हाथ में लिया है उन्हीं लोगों ने मोक्ष या निर्वाण को व्यक्ति के भविष्य में नहीं बल्कि अतीत में दिखाने वाले बाबाओं की सबसे बड़ी फौज को खड़ा करके उसका इस्तेमाल किया है।
गौर से देखिए, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो लोग भारत को एक धर्म विशेष के आधिपत्य में धकेलना चाहते हैं वे सबसे पहले किसी सतयुग को अतीत में खड़ा करते हैं। फिर वे उन बाबाओं और आध्यात्मिक व्याख्याओं का सहारा लेते हैं जो सब तरह के विकास को नकारकर अतीत की आदिम सुरंगों मे वैराग्य, कायाक्लेश, कायोत्सर्ग आदि से जुड़ी मोक्ष की धारणा सिखाते हैं।
ये दोनों रणनीतियाँ एक ही दिशा मे एकसाथ जाती हैं। इस खेल में चलताऊ बाबा ही नहीं बल्कि विवेकानंद, अरबिंदो घोष जैसे स्थापित गुरु और आजकल के ओशो रजनीश और जग्गी बाबा जैसे कल्ट गुरु भी खतरनाक खेल खेलते आए हैं। यह खेल अब अपने शिखर पर पहुँच गया है। इसीलिए आजकल बाबाओं और राजनेताओं में बड़ा भाईचारा नजर आता है।
इस तरह वे लोग जो अतीत में सतयुग और निर्वाण/मोक्ष देखते हैं वे लोग अचानक ही एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बनकर खड़े हो जाते हैं। यह सबसे गहरा खेल है जिसका इलाज चलताऊ प्रगतिशीलता और जिंदाबाद मुर्दाबाद के जरिए किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
इसका अब क्या किया जाए?
असल समस्या यह है कि आपके समाज में इंसान के जीवन और उसके मौलिक स्वरूप सहित सुख दुख और मोक्ष या निर्वाण की व्याख्या कौन और किस तरह कर रहा है। यह सबसे गंभीर और सूक्ष्म बात है।
अब भारत के बहुजनों को ठीक से समझना होगा कि राजनीतिक बदलावों के पीछे सामाजिक बदलावों का दबाव चाहिए और सामाजिक बदलावों के पीछे सांस्कृतिक धार्मिक बदलाव चाहिए।
भारत के बहुजन सैद्धांतिक रूप से राजनीतिक और सामाजिक बदलाव तक आ चुके हैं, अधिकांश ओबीसी चिंतक दलित और ट्राइबल चिंतक इस बात के प्रति सहमत हो चुके हैं कि राजनीतिक और सामाजिक बदलाव के लिए नई और साझा रणनीति की जरूरत है।
लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी ओबीसी, दलित और ट्राइबल समाज भारत में एकमुश्त धार्मिक और आध्यात्मिक बदलाव लाने की दिशा में पहला कदम भी नहीं उठाया गया है।
धर्म और अध्यात्म किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है। इसे नजरअंदाज करना आजकल की चलताऊ प्रगतिशीलता का पसंदीदा खेल बन गया है। जो प्रस्तावनाएं स्वयं को आधुनिक और प्रगतिशील कहती हैं वे धर्म और आध्यात्म की शक्ति को नकारते हुए भारत के बहुजनों का सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं।
यह एक षडय़ंत्र है जिसमें बहुजनों के सबसे जागरूक और शिक्षित लोग सबसे आसानी से फँसते आए हैं।
धर्म और अध्यात्म की शक्ति और उसके सही इस्तेमाल की संभावना को गैर-बहुजनों के हाथों में दे देने से बहुजन समाज अपने कल्याण के लिए उपयोगी सबसे शक्तिशाली उपकरणों से वंचित हो जाता है।
फिर इन उपकरणों का प्रयोग फिर गैर-बहुजन या अल्पजन करते हैं, और यह इस्तेमाल वे फिर अपने हितों के लिए करते हैं। अब इसमें अल्पजनों को जिम्मेदार ठहराने का कोई मतलब नहीं, जिम्मेदारी उन बहुजनों पर डाली जानी चाहिए जो धर्म और अध्यात्म की शक्ति का इस्तेमाल करने से इनकार करते आए हैं या फिर जिनमें इस इस्तेमाल की कल्पना, समझ और योग्यता नहीं है।
यह बात नोट करके रख लीजिए, भारत को वास्तव में वे लोग बदलेंगे जिन्हें खुद के जीवन मे निर्णायक बदलाव की जरूरत है। वे लोग भारत के बहुजन अर्थात ओबीसी, दलित और ट्राइब्स हैं। इसी बहुजन तबके को इस देश में धार्मिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बदलाव की निर्णायक पहल करनी होगी। जब तक भारतीय बहुजनों के घर घर में नए धर्म की नई इबारत नहीं पहुँच जाती तब तक लोकतंत्र और समाज में कोई ठोस और निर्णायक बदलाव नहीं आने वाला है।
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
हमारे सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार के बीच जजों की नियुक्ति पर जो खींचातानी चल रही थी, वह खुले-आम बाजार में आ गई है। सर्वोच्च न्यायालय के चयन-मंडल ने सरकार को जो नाम भेजे थे, उनमें से कुछ पर सरकार ने कई आपत्तियाँ की थीं। इन आपत्तियों को प्रायः गोपनीय माना जाता है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें जग-जाहिर कर दिया है। इस कदम से यह भी पता चलता है कि भारत में किसी भी उच्च पद पर नियुक्त होनेवाले जजों की नियुक्ति में कितनी सावधानी से काम लिया जाता है।
इस बार यह सावधानी जरा जरूरत से ज्यादा दिखाई पड़ी है, क्योंकि एक जज को इसलिए नियुक्त नहीं किया जा रहा है कि वह समलैंगिक है और दूसरे जज को इसलिए कि उसने ट्वीट पर कई बार सरकारी नीतियों का दो-टूक विरोध किया है। जहां तक दूसरे जज का सवाल है, सरकार की आपत्ति से सहमत होना ज़रा मुश्किल है। क्या सोमशेखर सुंदरेशन ने वे सरकार विरोधी ट्वीट जज रहते हुए किए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे जज थे ही नहीं। तब वे वकील थे और अब भी वकील हैं।
यदि एक वकील किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपनी राय जाहिर नहीं करेगा तो कौन करेगा? भारतीय नागरिक के नाते उसे भी अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है। हाँ, अब जज के नाते उन्हें अपनी अभिव्यक्ति पर संयम रखना होगा। सरकार का डर स्वाभाविक है लेकिन उनकी नियुक्ति के पहले उन्हें चेतावनी दी जा सकती है। उनकी नियुक्ति के विरोध से सरकार अपनी ही छवि खराब कर रही है। क्या इसका संदेश यह नहीं निकल रहा है कि सरकार सभी पदों पर ‘जी हुजूरों’ को चाहती है? दू
सरे जज पर यह आपत्ति है कि वह समलैंगिक है और उसका सहवासी एक स्विस नागरिक है। समलैंगिकता न्याय-प्रक्रिया में बाधक कैसे है, यह कोई बताए? दुनिया के कई राजा-महाराजा और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समलैंगिक रहे हैं। जहां तक उस जज के सहवासी का विदेशी होना है, कौन नहीं जानता कि भारत के एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, एक विदेश मंत्री और कई अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण लोगों की पत्नियां या पति विदेशी रहे हैं। यह तो मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह रहा हूं लेकिन यदि हम खोजने चलें तो ऐसे सैकड़ों मामले सामने आ सकते हैं।
यह ठीक है कि ऐसा होना कोई आदर्श स्थिति नहीं है लेकिन आज की दुनिया इतनी छोटी हो चुकी है कि इस तरह के मामले बढ़ते ही चले जाएंगे। भारतीय मूल के लोग आजकल दुनिया के लगभग दर्जन भर देशों में उनके सर्वोच्च पदों पर प्रतिष्ठित हैं या नहीं? बेहतर तो यही होगा कि चयन-मंडल (कालेजियम) का स्वरूप ही बदला जाए और अगर यह फिलहाल नहीं बदलता है तो सरकार और सर्वोच्च न्यायालय में चल रही मुठभेड़ तुरंत रूके। वरना, दोनों की सही कार्रवाइयों को भी जनता मुठभेड़ का चश्मा चढ़ाकर देखेगी। (नया इंडिया की अनुमति से)
-राजशेखर चौबे
किसी ने भी यह नहीं कहा कि कद में क्या रखा है परंतु जिनका बड़ा नाम है वे ही कह कर चले गए - नाम में क्या रखा है ? खुद तो नाम कमा कर चले गए और दूसरों को ज्ञान बांट गए। यह भी कहा गया है- बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर....। यहां बड़ा का अर्थ बड़ा नहीं ऊँचा है। किसी ने शायद यह भी नहीं कहा कि ऊंचा होने में क्या रखा है. अब ऊंचाई अधिक होने का अर्थ है अधिक ऊंचा होना या कुलीन होना। ऊंचे लोग ऊंची पसंद। बॉलीवुड, टॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक ऊंचे या लंबे हीरो हीरोइनों का बोलबाला है । ऊंचे लोगों के अधिक सफल होने के दावे भी किए जाते हैं । वैसे ये हीरो हीरोइन भारी मेकअप के साथ-साथ अंदरूनी हील वाले जूते सैंडल आदि पहनते हैं जिनसे इनकी ऊंचाई तीन से छह इंच तक बढ़ जाती है । अब केवल हीरो हीरोइन ही नहीं तमाम वे लोग जो ऊंचे ब्रांड की चीजों का इस्तेमाल करते हैं , अपनी ऊंचाई तीन से छह इंच तक बढ़ा सकते हैं । आप केवल साठ लाख खर्च में ऑपरेशन करवाकर अपनी टांगों की लंबाई तीन से छह इंच तक बढ़वा सकते हैं । इस ऑपरेशन से केवल टांगों की लंबाई बढ़ती है किसी दूसरे अंग की नहीं । इससे भी कुछ अति उत्साही लोग दुखी हो गए हैं । यदि ऑपरेशन से हाथों की लंबाई बढ़ती तो आजानुबाहु लोगों की संख्या में वृद्धि दर्ज हो जाती। महिलाओं में सुंदरता का क्रेज है और पुरुषों में रोबीला होने का अत: पुरुषों का झुकाव इस ऑपरेशन की ओर अधिक है । टेक कर्मचारी गिव एंड टेक में भरोसा रखते हैं इसीलिए वे ही सबसे ज्यादा इस ऑपरेशन को करवा रहे हैं । अब राजपाल सुल्तान की ऊंचाई पा सकते हैं और सुल्तान अपनी पूर्व प्रेमिका के ससुर की ऊंचाई पा सकते हैं । आलिया भी कैटरीना की ऊंचाई हासिल कर अपने पति को खुश कर सकती है । ब्रेस्ट का साइज बढ़ाने के लिए सर्जरी होती रही है लेकिन अभी तक ऐसी सर्जरी नहीं हुई है जो सीने को 36 इंच से 56 इंच का कर दे । यदि ऐसा कोई ऑपरेशन होने लगे तो नेताओं की लाइन लग जाएगी । तब यह भी संभव है कि 56 इंच वाले अपना सीना 76 इंच करवा ले । अति उत्साही और महत्वाकांक्षी राजनीति में ही नहीं बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं और साहित्य भी अपवाद नहीं है।
ऐसे ही एक लेखक अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो ऑपरेशन करवाकर अपनी ऊंचाई बढ़वा लें और बड़े कद के लेखक बन जाए । राम जाने बड़े कद के लेखक बनने की उनकी यह अभिलाषा कब पूरी होगी ? वैसे भी इन दिनों बहुत सारे साहित्यकार बड़े कद के लेखक बनने के लिए अमेरिका गए हुए हैं।मैं भी बड़े कद का लेखक बनने के लिए अमेरिका प्रस्थान कर रहा हूँ।क्या आप भी बड़े कद के लेखक बनना चाहते हैं तो आप भी अमेरिका प्रस्थान की तैयारी कीजिए।
-अरूण कान्त शुक्ला
कोरोना के कारण शिक्षा पर क्या असर पड़ा ये किसी से छुपा नहीं है, ऑनलाइन क्लासेज की वजह से बच्चों की शारीरिक क्षमता पर असर पडऩे लगा था, जिस पर उस दौरान संबंधित अभिभावकों सहित सभी पक्षों ने चिंता भी जाहिर की थी। ये चिंताएं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और सरकारी शिक्ष्ण संस्थाओं में पढने वाले छात्रों को लेकर अधिक थीं क्योंकि ग्रमीण क्षेत्रों के अभिभावकों के पास ऑन लाइन शिक्षण के लिए मोबाइल या लेपटॉप जैसी अन्य सुविधा के अभाव के साथ साथ अबाध इंटरनेट की उपलब्धता भी एक समस्या न केवल अभिभावकों बल्कि शिक्षकों के लिये भी थी। इसीलिये जब स्कूल खुले तो अभिभावकों और छात्रों के साथ शिक्षकों में भी उत्साह देखने मिला था। इन सभी परिस्थितियों की बच्चों की मानसिक स्थिति तथा शारीरिक क्षमता पर कितना असर पड़ा और उनकी बच्चों की पढने तथा समझने और शिक्षकों की पढ़ाने की क्षमता में क्या फर्क आया, इस पर एक स्वतन्त्र सर्वे बहुत आवश्यक हो गया था ताकि उस आधार पर संबंधित पक्ष छात्रों के अध्यन के लिये उचित तरीकों का निर्धारण कर सकें।
अब इसे तरह के सभी बिन्दुओं को समेटते हुए एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन (्रस्श्वक्र 2022) की रिपोर्ट बुधवार 18 जनवरी को जारी की गई है। प्रथम फाउंडेशन की ओर से चार साल बाद यह सर्वेक्षण किया गया है। इससे पहले साल 2018 में असर की रिपोर्ट जारी की गई थी।
साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 780 जि़ले और 6 लाख 40 हज़ार 867 गांव हैं जिसमें ‘असर’ ने 616 ग्रामीण जि़लों के 19,060 गांवों का सर्वे किया है, इसमें 3 से 16 वर्ष तक की आयु वाले 6.9 लाख बच्चों को शामिल किया गया है ताकि उनकी स्कूली शिक्षा की स्थिति दर्ज की जा सके और उनकी बुनियादी पढ़ाई और समझ का आंकलन किया जा सके।
कोरोना के बाद बढ़े नामांकन
राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की स्थिति को देखकर पता चलता है कि महामारी के दौरान स्कूल बंद हो जाने के बावजूद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का नामांकन दर पिछले 15 सालों में 95 प्रतिशत से ज़्यादा रहा है। याने वर्ष 2018 में यह 95.2 प्रतिशत था, जो अब बढक़र 98.4 प्रतिशत हो गया है।
3-16 आयु वर्ग के वो बच्चे जिनका वर्तमान में नामांकन दर्ज नहीं है, इनका अनुपात भी जो वर्ष 2018 में 2.8 प्रतिशत था अब घटकर अब 1.6 प्रतिशत रह गया है याने कोरोना के बाद शालाओं में नामांकन बढ़ा है।
सरकारी स्कूलों में नामांकन
सर्वे में पाया गया की सरकारी स्कूलों में 2018 के मुक़ाबले 2022 में तेज़ी से नामांकन हुए हैं, यानी जो नामांकन प्रतिशत 2018 में 65.6 था वो 2022 में बढक़र 72.9 प्रतिशत हो गया है। हालांकि इससे पहले साल 2006 से 2014 तक सरकारी विद्यालयों में नामांकन की दर बेहद कम थी। असर की वर्ष 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक़ ये आंकड़ा तब 64.9 प्रतिशत था जो अगले चार सालों तक वैसा ही बना रहा।
बच्चों की बुनियादी साक्षरता, समझ और आंकलन करने की क्षमता में बड़ी गिरावट
कोरोना के कारण लंबे वक्त तक शिक्षण व्यवस्था अन्य सभी व्यवस्थाओं की तरह पुरी तरह ठप्प थी, बल्कि सचाई तो यह है कि यह कुछ अधिक लम्बी अवधी तक व्यवस्थित नहीं हो पाई थी। परिणाम स्वरूप बच्चों की बुनियादी साक्षरता, समझ और आंकलन करने की क्षमता में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ये सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होता है।
कक्षा 3 की हालत : असर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में कक्षा तीन के बच्चों का प्रतिशत जो कक्षा दो के स्तर के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते थे 27.3 प्रतिशत था जो अब वर्ष 2022 में गिरकर 20.5 रह गया है।
2018 के स्तर से 10 प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट दिखाने वाले राज्यों की बात करें तो केरल 2018 में 52.1 प्रतिशत से 2022 में 38.7 प्रतिशत तक, हिमाचल प्रदेश 47.7 प्रतिशत से 28.4 प्रतिशत तक और हरियाणा में 46.4 प्रतिशत से 31.5 प्रतिशत तक गिरावट आई है।
कक्षा 5 की हालत- असर की रिपोर्ट कहती है कि चाहे वे स्कूल सरकारी हों अथवा प्राईवेट सर्वे में दोनों की हालत दयनीय ही है।
कक्षा पांच में नामांकित बच्चों का अनुपात जो कि कम से कम कक्षा दो के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं, वो 2018 के 50.5 प्रतिशत से गिरकर 2022 में 42.8 प्रतिशत हो गया।
हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्हें ठीकठाक कहा जा सकता है, इनमें बिहार, ओडिशा, मणिपुर और झारखंड के अलावा कुछ और राज्य शामिल हैं। वहीं, 15 प्रतिशत अंकों या उससे ज़्यादा की कमी वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। जबकि उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 10 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखी गई है।
आठवीं कक्षा के क्या हालात- रिपोर्ट कहती है कि कक्षा आठवीं के छात्रों में बुनियादी पढऩे की क्षमता में कमी तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि तीन और पांच कक्षा में देखे गए रुझानों की तुलना में थोड़ा कम हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, सरकारी या निजी स्कूलों में कक्षा आठ में नामांकित 69.6 प्रतिशत बच्चे 2022 में कम से कम बुनियादी पाठ पढ़ सकते हैं, जो 2018 में 72.8 प्रतिशत था।
‘घटाना’ नहीं आता- गणित की भाषा में कहें तो कक्षा 3 के वो छात्र जो कम से कम ‘घटाव’ जानते हैं, उनके प्रतिशत में भी गिरावट आई है। यानी ऐसे बच्चों की जो संख्या साल 2018 में 28.2 प्रतिशत थी वो 2022 में 25.9 प्रतिशत हो गई है। हालांकि जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में इनके आंकड़ों ने थोड़ी राहत ज़रूर दी है। इन तीनों राज्यों में आंकड़े लगभग स्थिर हैं। जबकि हरियाणा, मिज़ोरम और तमिलनाडु में कऱीब 10 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है।
तमिलनाडु में 2018 में ये प्रतिशत 25.9 था जो 2022 में 11.2 हो गया, मिजोरम में 2018 में इसकी संख्या 58.9 थी जो 2022 में घटकर 42 प्रतिशत हो गई, जबकि हरियाणा में भी 10 फ़ीसदी गिरकर 41.8 प्रतिशत हो गई जो 2018 में 53.9 थी।
‘भाग’ के सवाल से भी दिक्कत पर सरकारी स्कूलों में किंचित सुधार- असर की रिपोर्ट कक्षा 8 के बारे में कहती है कि बुनियादी गणित के मामले में प्रदर्शन थोड़ा अलग है। राष्ट्रीय स्तर पर भाग का सवाल हल कर पाने वाले बच्चों का अनुपात थोड़ा बेहतर हुआ है। ये 2018 में 44.1 प्रतिशत था, जबकि 2022 में 44.7 प्रतिशत हो गया है। रिपोर्ट कहती है कि ये जो बहुत थोड़ी सी बढ़ोत्तरी है ये लड़कियों और सरकारी स्कूल के बच्चों की ज़्यादा सीखने की इच्छा के कारण हुआ है। जबकि ‘भाग’ बनाने के सवालों में लडक़ों और निजी स्कूलों की क्षमता में गिरावट हुई है।
प्राइवेट ट्यूशन का बोलबाला- ग्रामीण भारत में कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने के मामले में भी बढ़ोत्तरी हुई है। सरकारी हो या ग़ैर सरकारी, दोनों ही स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है। फीस देकर ट्यूशन पढऩे वालों का अनुपात साल 2018 में 26.4 प्रतिशत से बढक़र 2022 में 30.5 प्रतिशत हो गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में तो 8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।
स्कूलों में सुविधाएं- लड़कियों के शौचालय का जो अनुपात 2018 में 66.4 प्रतिशत था, वो 2022 में 68.4 प्रतिशत हुआ है, हालांकि जरूरी प्रसाधनों के हिसाब से इसे बहुत बड़ी वृद्धि नहीं कहा जा सकता। पेयजल वाले स्कूलों में भी वृद्धि देखने को मिली है, ये साल 2018 में 74.8 प्रतिशत थे जो 2022 में बढक़र 76 प्रतिशत हो गए।
हालांकि गुजरात जैसे राज्य में पेयजल वाले स्कूलों की संख्या में गिरावट आई है, यहां ये संख्या 88 प्रतिशत से घटकर 71.8 प्रतिशत हो गई है, और कर्नाटक में भी 76.8 प्रतिशत से घटकर 67.8 प्रतिशत हो गई है।
कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल किए गए सर्वे का तुलनात्मक विश्लेषण
शिक्षा के स्तर में आई उपरोक्त बड़ी गिरावटों के बावजूद, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में सीखने के परिणामों के तुलनात्मक विश्लेषण से सामने आया कि एक बार स्कूलों के फिर से खुलने के बाद इन राज्यों में खोई हुई जमीन को वापस पाने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ में, कक्षा 3 के बच्चों का अनुपात जो कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक पढ़ सकते हैं, जो 2018 में 29.8 प्रतिशत से नीचे था, 2021 में 12.3 प्रतिशत तक गिर गया था, वह 2022 में 24.2 प्रतिशत तक वापस आ गया। पश्चिम बंगाल में, यह 2021 में 29.5 प्रतिशत से बढक़र 2022 में 33 प्रतिशत हो गया।
गणित के मामले में, छत्तीसगढ़ में कक्षा 3 में बुनियादी गणित प्रश्नों को हल करने की क्षमता वाले बच्चों की हिस्सेदारी 2018 के 19.3त्न से गिरकर 2021 में 9त्न हो गई थी , जो 2022 में बढक़र 19.6त्न हो गई है। कर्नाटक में 2021 के 17.3त्न से बढक़र यह 2022 में 22.2त्न और पश्चिम बंगाल में 2021 के 29.4त्न से बढक़र 2022 में 34.2त्न हो गया है।
निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में दाखिले का रुझान : सर्वे में यह भी पाया गया कि ग्रमीण तथा अर्द्धशहरी स्थानों में निजी स्कूलों को छोडक़र सरकारी स्कूलों में नामांकन की तरफ रुझान बढ़ा है। प्रथम फाउंडेशन की सीईओ रुक्मिणी बनर्जी ने के अनुसार निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों की तरफ जाने का जो रुझान अभी दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे अनेक कारक रहे हैं, जिसमें महामारी की वजह से नौकरी छूटना और ग्रामीण क्षेत्रों में बजट की कमी की वजह से निजी स्कूलों का बंद होना भी शामिल है।
उनका कहना था कि अगर परिवार की आय कम हो जाती है या अधिक अनिश्चित हो जाती है, तो संभावना है कि माता-पिता निजी स्कूल की फीस वहन करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए उनके पास इसके अलावा अन्य कोई चारा नहीं होगा कि वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में दाखिल करायें। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में, अधिकांश निजी स्कूल कम लागत या कम बजट वाले ही होते हैं और उनमें से अनेक को कोविड के दौरान बंद करना पड़ा।
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
सन् 2023 में भारत के जिन नौ राज्यों में चुनाव होने हैं, उनका डंका बज गया है। उत्तर-पूर्व के तीन राज्यों- त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड में अगले माह चुनाव होनेवाले हैं। इन तीनों राज्यों में भाजपा स्वयं अपने दम पर सत्तारूढ़ नहीं है लेकिन तीनों में वह सत्तारूढ़ गठबंधन की सदस्य है। तीनों राज्यों की 60-60 विधानसभा सीटों पर फरवरी में चुनाव होने हैं। इन 60 सीटों में से 59 सीटें नगालैंड में, 55 मेघालय में और 20 त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।
इन राज्यों में कुल मतदाताओं की संख्या सिर्फ 6 लाख 28 हजार है लेकिन शेष राज्यों में होनेवाले चुनाव भी इन राज्यों के चुनाव परिणामों से कुछ न कुछ प्रभावित जरूर होंगे। भाजपा की मन्शा है कि जैसे उत्तर भारत के राज्यों और केंद्र में भाजपा का नगाड़ा बज रहा है, वैसे ही सीमांत के इन प्रांतों में भी भाजपा का ध्वज फहराए। इसीलिए भाजपा के चोटी के नेता कई बार इस दूर-दराज के इलाके में अपना प्रभाव जमाने के लिए जाते रहे हैं। इन तीनों राज्यों की गठबंधन सरकारों में शामिल हर बड़े दल की इच्छा है कि इस बार वह स्पष्ट बहुमत प्राप्त करे और अकेला ही सत्तारूढ़ हो जाए।
जो भाजपा का लक्ष्य है, वह ही बाकी सभी का लक्ष्य है। जाहिर है कि वे दल भाजपा के मुकाबले ज्यादा मजबूत हैं। उनका जनाधार काफी बड़ा है लेकिन इन सीमांत राज्यों की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यह रही है कि केंद्र में जो भी सरकार बने, वे उसके रंग में रंग जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे अपनी अर्थ-व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार की दया पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि इन सारे स्थानीय दलों के नेता टूट-फूटकर भाजपा में शामिल हो जाएं और वहां भाजपा की सरकारें बन जाएं।
भाजपा इस लक्ष्य को पाने पर इतनी आमादा है कि प्रधानमंत्री ने अपने पिछले पार्टी-अधिवेशन में मुसलमानों और ईसाइयों के भले की बात उठाई है। गोमांस-भक्षण पर भी संघ और भाजपा ने कड़ा रूख नहीं अपनाया है। ईसाई मतदाता इस इलाके में बहुत ज्यादा हैं। वैसे इन राज्यों में यदि सभी सरकारें भाजपा की बन गईं तो यह भरोसा नहीं है कि शेष राज्यों में भी उसी की सरकारें बनेंगी, क्योंकि हर राज्य के अपने-अपने राजनीतिक समीकरण हैं।
तेलंगाना में हुए विशाल जन-प्रदर्शन में कम्युनिस्ट, समाजवादी और आप पार्टियों के नेताओं ने विरोधी गठबंधन का बिगुल काफी जोर से बजाया है लेकिन इस गठबंधन से कांग्रेस, ममता बनर्जी, नीतीशकुमार, कुमारस्वामी जैसे विपक्षी नेता अभी भी बाहर हैं। यदि यही हाल जारी रहा तो भाजपा का पाया अगले चुनावों में भी मजबूत बनकर उभरेगा। (नया इंडिया की अनुमति से)
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
इस बार भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है, उसकी भूमिका एतिहासिक हो सकती है, बशर्ते कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, उस पर अमल किया जाए। मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत के मंत्र को अमली जामा पहनाने की बात कही है। मोहनजी बार-बार कह चुके हैं कि हिंदू-मुसलमानों का डीएनए एक ही है। मोदी ने इसी मंत्र को व्यावहारिक रूप देते हुए कहा है कि पसमांदा वर्ग के अल्पसंख्यकों याने मुसलमानों, केरल के ईसाइयों और देश के पिछड़े लोगों को साथ लेकर चलने का संकल्प किया जाना चाहिए। भाजपा के प्रधानमंत्री और संघ के तपस्वी स्वयंसेवक के मुंह से ऐसी बात सुनकर कौन गदगद नहीं हो जाएगा?
मैं पिछले तीन-चार दिन से दुबई और अबू धाबी में कई अरब शेखों से मिला और हमारी सभी पार्टियों व विचारधाराओं के लोगों से मेरा खुला संवाद हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जिन लोगों के पास दूरदृष्ष्टि है, वे यह महसूस करते हैं कि यदि भारत में सांप्रदायिक दुर्भाव चलता रहा तो अगले 50-60 साल में भारत के इस बार फिर दो नहीं, सौ टुकड़े भी हो सकते हैं। इस आशंका को निरस्त करने का शंखनाद भाजपा ने अब कर दिया है। यदि भाजपा सरकार सांप्रदायिक सदभाव पैदा करने और देश के पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बुनियादी उपायों पर ध्यान दे तो भारत सिर्फ एक दशक में ही दुनिया का महासंपन्न और महाशक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है। भारत का दुर्भाग्य यह रहा कि हमारी अब तक की सरकारों के नेताओं को वह चाबी हाथ ही नहीं लगी, जो सदियों से बंद पड़े भारत के ताले को खोल सकती है। वह चाबी है, शिक्षा और चिकित्सा में मूल सुधार ताकि देश का मन और तन बलवान बन जाए। ये मूल सुधार करने की बजाय हमारी सभी सरकारें रेवड़ियां बांटने की चुनावी रणनीतियां अपनाती रही हैं। मोदी सरकार ने इस मामले में भी जबर्दस्त उस्तादी दिखाई है। मोदी ने कहा है कि हमें वोटों के लिए नहीं, लेकिन राष्ट्रीय सुद्दढ़ता के लिए मुसलमानों, ईसाइयों और पिछड़ों की सेवा करनी है। यह बात तो अति उत्तम है लेकिन इसे ठोस रूप कैसे देंगे? इसे समझने के लिए हमारे नेताओं में इतनी विनम्रता होनी चाहिए कि वे चिंतकों और बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर खुला संवाद करें।
सिर्फ नौकरशाहों के इशारों पर नाचने से आप सत्ता तो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन देश की दशा नहीं बदल सकते। भाजपा के अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा को लगातार दूसरी बार भी अध्यक्ष पद से सम्मानित किया गया है, यह सर्वथा उचित है, क्योंकि वे ऐसे पार्टी-अध्यक्ष हैं, प्रायः जिनके बयान और आचरण आपत्तिजनक और कटु विवादास्पद नहीं होते हैं और जो सभी को साथ लेकर चलने की इच्छा रखते हैं। अब प्रधानमंत्री से भी ज्यादा उनकी जिम्मेदारी है कि वे भाजपा को एक ऐसा रूप प्रदान करें, जो आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस का रहा है। यदि भाजपा सर्वसमावेशी बन जाए और बुनियादी परिवर्तनों पर ध्यान दे तो दुनिया की वर्तमान सदी भारत की सदी बन सकती है। (नया इंडिया की अनुमति से)
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ आजकल प्रधानमंत्री कम, प्रधानभिक्षु बनकर देश-विदेश के चक्कर लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्हें सउदी अरब जाकर अपना भिक्षा-पात्र फैलाना पड़ा। तीन-चार दिन पहले वे अबू धाबी और दुबई आए हुए थे। संयोग की बात है कि दो-तीन दिन के लिए मैं भी दुबई और अबू धाबी में हूं। यहां के कई अरबी नेताओं से मेरी बात हुई। पाकिस्तान की दुर्दशा से वे बहुत दुखी हैं लेकिन वे पाकिस्तान पर कर्ज लादने के अलावा क्या कर सकते हैं?
उन्होंने 2 बिलियन डाॅलर जो पहले दे रखे थे, उनके भुगतान की तिथि आगे बढ़ा दी है और संकट से लड़ने के लिए 1 बिलियन डाॅलर और दे दिए हैं। शाहबाज़ की झोली को पिछले हफ्ते भरने में सउदी अरब ने भी काफी उदारता दिखाई थी। लेकिन पाकिस्तान की झोली में इतने बड़े-बड़े छेद हैं कि ये पश्चिम एशियाई राष्ट्र तो क्या, उसे चीन और अमेरिका भी नहीं भर सकते। इन छेदों का कारण क्या है? इनका असली कारण है- भारत।
भारत के विरूद्ध पाकिस्तान की फौज और सरकार ने इतनी नफरत कूट-कूटकर भर दी है कि उस राष्ट्र का ध्यान खुद को संभालने पर बहुत कम लग पाता है। इसी नफरत के दम पर पाकिस्तानी नेता चुनावों में अपनी गोटी गरम करते हैं। वे कश्मीर का राग अलापते रहते हैं और फौज को अपने सिर पर चढ़ाए रखते हैं। आम जनता रोटियों को तरसती रहती है लेकिन उसे भी नफरत के गुलाब जामुन कश्मीर की तश्तरी में रखकर पेश कर दिए जाते हैं। पिछले हफ्ते शाहबाज शरीफ, कजाकिस्तान और संयुक्त अरब अमारात गए। वहां भी उन्होंने कश्मीर का राग अलापा।
उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से बात करने की पहल की, जो कि अच्छी बात है लेकिन साथ में ही यह धमकी भी दे डाली कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हो गया तो कोई नहीं बचेगा। दोनों के पास परमाणु बम हैं। शाहबाज ने अबू धाबी के शासक से कहा कि भारत से आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप मध्यस्थता क्यों नहीं करते? एक तरफ वे मध्यस्थता की बात करते हैं और दूसरी तरफ, वे भारत से कहते हैं कि आप संयुक्तराष्ट्र संघ के प्रस्ताव के मुताबिक कश्मीर हमारे हवाले कर दो।
पाकिस्तान के दो-तीन प्रधानमंत्रियों से मेरी बहुत ही मैत्रीपूर्ण बातचीत में मुझे पता चला कि उन्होंने संयुक्तराष्ट्र के उस प्रस्ताव का मूलपाठ कभी पढ़ा ही नहीं है। उन्हें यह पता ही नहीं है कि उस प्रस्ताव में कहा गया है कि पाकिस्तान पहले तथाकथित ‘आज़ाद कश्मीर’ को खाली करे। शाहबाज को चाहिए था कि वे आतंकवाद के विरूद्ध भी कुछ बोलें। लेकिन ऐसा लगता है कि अबू धाबी में उन्होंने जो कुछ कहा है, वह यहां के शासकों को खुश करने के लिए कहा है।
यह शाहबाज़ शरीफ की ही नहीं, सभी पाकिस्तानी नेताओं की मजबूरी है कि जो लोग उनकी झोली में कुछ जूठन डाल देते हैं, उन्हें कुछ न कुछ महत्व तो देना ही पड़ता है। आखिर में खाली भिक्षा-पात्र को भरा जाना ही है, हर शर्त पर! इसीलिए दोनों नेताओं के संयुक्त वक्तव्य में शाहबाज़ के उक्त बयान का जिक्र तक नहीं है। (नया इंडिया की अनुमति से)
-गीता प्रसाद
आप किसी भी लडक़े से उसका पसंदीदा रंग पूछिए, उत्तर में आपको अधिकतर नीला, काला, सफेद, ग्रे या खाकी जैसे रंगों का ही जि़क्र मिलेगा। अच्छा ये बताइए, आपने कितने लडक़ों को गुलाबी शर्ट या टीशर्ट पहने देखा है?
शायद एक भी नहीं। तो क्या उन्हें गुलाबी रंग से कुछ परहेज है? किसी भी रंग के प्रति हमारी रुचि या अरुचि, हमारे व्यक्तित्व और गुणों के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो क्या गुलाबी रंग जो कि कोमलता, सौम्यता, मृदुलता का प्रतीक है; क्या ये सभी गुण लडक़ों में उपस्थित नहीं?
इसका उत्तर मैंने खोजने का प्रयास किया... पहलेपहल मुझे बमुश्किल एक ही चेहरा याद आया। थोड़ा और चिंतन करने के बाद मुझे बहुत सारे ‘गुलाबी लडक़े’ नजर आने लगे। वो लडक़े, जिन्होंने गुलाबी रंग को भले ही अपने वॉर्डरोब में जगह न दी हो, मगर उसे सदैव अपने हृदय में संचित, पोषित और जीवित रखा है।
मेरे ख्याल में... गुलाबी हैं वो लडक़े, जो आज भी हर लडक़ी को दिल तो क्या, दिल वाली इमोजी भी भेजने में कई बार सोचते हैं।
गुलाबी हैं वो लडक़े, जो घर में बहनों के अभाव में मेहमानों के लिए सलीके से ट्रे में पानी ले आते हैं। गुलाबी हैं वो लडक़े जिन्हें कभी मां-बाप, बहन- भाई की, गाली देना नहीं आया।
गुलाबी हैं वो लडक़े भी, जो रसोई से खाना लेते समय अक्सर देख लिया करते कि मां के लिए सब खत्म ना हो जाए ।
गुलाबी हैं वो लडक़े भी, जो अपनी दोस्त के पहले क्रश की कहानियां ध्यान से सुनते और उनसे कभी नहीं कहते कि वह भी उनसे प्यार कर बैठे हैं।
मैं कहती हूँ, बहुत गुलाबी हैं वो लडक़े, जिन्होंने लोकल ट्रेन या राह चलते किसी लडक़ी को छेड़छाड़ से बचाया है।
और बहुत बहुत गुलाबी हैं वो लडक़े जिन्होंने, किसी बलात्कार या एसिड अटैक विक्टिम से प्रेम या विवाह किया।
गुलाबी हैं वो लडक़े भी तो जिनकी आँखें, अपनी दोस्त, प्रेमिका या पत्नी के सामने अपने कठिन दौर को याद करते समय नम हो गयीं।
सुनो, गुलाबी हैं वो लडक़े भी, जो खुद चाय प्रेमी ना होने के बावजूद, कामकाजी पार्टनर के लिए एक कप चाय बनाने की नापतौल में, रोज़ डेढ़ कप चाय बना बैठते और बेमन से ही सही, रोज आधा कप चाय संग में पी लिया करते। और यक़ीन मानिए, गुलाबी थे, हैं और हमेशा रहेंगे, वो लडक़े ... जो अपनी पहली संतान एक बेटी चाहते हैं, जो बिल्कुल उनके जैसी दिखती हो।
मैं दावे से कह सकती हूँ कि ये ‘गुलाबी लडक़े’ किसी के भी जीवन को हर रंग से भरने में सक्षम हैं। दिल से शुक्रिया...! सभी ‘गुलाबी लडक़ों’ का..., बाहर से चाहे जैसे दिखो, मगर सदैव बचाये रखना इस गुलाबी रंग को अपने कोमलतम हृदय में...!!!
-डॉ. संजय शुक्ला
आर्थिक उदारीकरण और संचार क्रांति ने सबसे ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन सूचना माध्यमों में लाया है लेकिन इसका नाकारात्मक स्वरूप भी सामने है। हाल ही में देश के शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट के दो सदस्यीय बेंच ने ‘हेट स्पीच’ पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि भारत में टेलीविजन न्यूज चैनल समाज में दरार पैदा कर रहे हैं तथा ये चैनल अपने नियत एजेंडे पर चलते हैं। जजों ने यह भी कहा कि ये चैनल्स सनसनीखेज खबरों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा अपने एजेंडे के तहत नफरत फैलाने वाले खबरें प्रसारित करते हैं। अदालत ने समाचार एंकरों के खिलाफ कार्रवाई की मंशा जाहिर करते हुए यह भी कहा कि नफरती भाषण एक राक्षस है जो सबको निगल जाएगा।पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि समाज में नफरत फैलाने वाले प्रसारण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? जवाब में सरकार ने कहा है कि नफरती भाषण से निबटने के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 'सीआरपीसी' में व्यापक संशोधन की योजना बनाई जा रही है। हालांकि सरकार अदालत को ऐसा भरोसा बीते कई सालों से दे रही है लेकिन नतीजा सिफर ही है।
बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सच की अभिव्यक्ति है जिसे बहुसंख्यक देशवासी महसूस कर रहे हैं। यह कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि पत्रकारिता की मर्यादा और जवाबदेही को सबसे ज्यादा खंडित इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल्स ने ही किया है जो टीआरपी की भूख मिटाने किसी भी सीमा को लांघने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। भारत में पत्रकारिता का एक उजला इतिहास रहा है जिसने देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वातंत्र्योत्तर भारत में अपनी प्रतिष्ठापूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है फलस्वरूप मीडिया यानि पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दर्जा दिया गया। हाल के वर्षों में जब समूचे समाज में नैतिक मूल्यों का क्षरण बड़ी तेजी से हो रहा है तब पत्रकारिता भी इससे अछूता नहीं है। मीडिया में जारी अधोपतन का खामियाजा देश के उस तबके को भोगना पड़ रहा है जिसके लिए खबरिया चैनल ?????आंख और कान हैं। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि मीडिया जगत में जारी भरोसे के संकट के बीच आज भी प्रिंट मीडिया यानि अखबारों के प्रति लोगों में विश्वसनीयता कायम है। बहरहाल संचार क्रांति के इस दौर में जब इंटरनेट आम आदमी के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है तब यह माध्यम फेक और नफरती खबरें बांटने में अव्वल साबित हो रहा है। गौरतलब है कि कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेब मीडिया पर फर्जी और लोगों को बदनाम करने वाली खबरों के चलन पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार को ऐसे खबरों को रोकने के लिए जरूरी उपाय करने का निर्देश दिए थे।
बीते सालों के दौरान अदालतों ने न्यूज चैनल्स के गैर जिम्मेदाराना रवैए पर क?ई बार सख्ती दिखाई थी लेकिन इस मनमानी पर अब तक रोक नहीं लग पाया है बिलाशक इसके लिए राजनीतिक संरक्षण ही जिम्मेदार है। हाल के वर्षों में मीडिया पर सत्ता प्रतिष्ठान को खुश रखने के लिए पक्षपाती होने और निष्पक्ष मीडिया हाउस के कर्ताधर्ताओं को सरकारी एजेंसियों के माध्यम से दबाव में लाने के आरोप लगातार लग रहे हैं। विपक्षी नेताओं की मानें तो देश में मीडिया पर अघोषित सेंसरशिप लागू है।दरअसल देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर टेलीविजन न्यूज चैनल ऐसी खबरें परोस रहीं हैं जिससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द लगातार बिगड़ रहा है फलस्वरूप कानून और व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है। एक न्यूज एजेंसी के सर्वे के मुताबिक टीवी चैनलों में शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक हो रहे बहसों में 70 फीसदी बहस धार्मिक, सांप्रदायिक, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों पर होते हैं। इन चैनलों में देश की ज्वलंत समस्या महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी और बीमारी पर कोई सार्थक बहस नहीं देखी गई।यह कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि मुल्क में मजहबी उन्माद फ़ैलाने के लिए जितना जिम्मेदार राजनीतिक और धार्मिक संगठन हैं उतना ही जिम्मेदार इलेक्ट्रॉनिक न्यूज मीडिया भी है।
अधिकांश टीवी चैनल्स में सलेक्टिव धार्मिक मुद्दों पर दोनों मजहबों के बीच हिंसा भडक़ाने और वैमनस्य बढ़ाने वाले निरर्थक बहस का चलन बढ़ा है। टीवी एंकर ऐसे पार्टी प्रवक्ताओं, मजहबी नेताओं, साधु-साध्वियों और मौलवियों को बैठाकर आक्रामक बहस के लिए प्रेरित करते हैं जिन्हें हिंदू धर्म या इस्लाम की भलिभांति जानकारी ही नहीं है और बल्कि वे एक नियत एजेंडे पर बहस करते हैं। गौरतलब है कि बीते साल नूपुर शर्मा विवाद के जड़ में भी ऐसा ही टीवी डिबेट था, इस बहस में एंकर की भूमिका गैर जिम्मेदाराना थी एंकर चाहती तो नुपुर शर्मा को आपत्तिजनक टिप्पणियां करने से रोक सकती थीं अथवा खुद टीवी चैनल भी इस प्रसारण को रोक सकती थीं लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बहस का परिणाम आज भी देश भोग रहा है और विदेशों में भारत की छवि अलग प्रभावित हुई। इन टीवी चैनलों के पक्षपाती रवैए की झलक विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर होने वाले चर्चा के दौरान भी दिखाई पड़ती है जब टीवी एंकर सत्ता से जुड़े राजनीतिक दल के प्रवक्ता को अपनी बात रखने के लिए सुविधाजनक समय देते हैं लेकिन विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं के तर्क और तथ्य रखने के दौरान कभी समय का बहाना बना कर अथवा ब्रेक लेकर उनके साथ पक्षपात करते हैं। आलम यह रहता है कि अनेक बार खुद एंकर विपक्षी प्रवक्ताओं पर हावी होने की कोशिश करते हैं जो किसी भी लिहाज से स्वस्थ पत्रकारिता नहीं है। अलबत्ता टीवी चैनलों के बहस में केवल धर्म और साम्प्रदायिकता पर ही भडक़ाऊ बातें नहीं की जा रही है बल्कि देश के संविधान, अदालतों, जांच एजेंसियों और विपक्षी नेताओं के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही है। टीवी चैनल किसी मामले पर जिस तरह मीडिया ट्रायल प्रसारित करतीं हैं मानो देश में अब पुलिस और अदालतों की कोई जरूरत ही नहीं रह गई है। फिल्म अभिनेता सुशांत राजपूत के आत्महत्या और शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान से संबंधित ड्रग्स मामले में टीवी चैनलों के मीडिया ट्रायल ने पुलिस और अदालत को भी हैरत में डाल दिया था जबकि नतीजा कुछ और निकला। नवंबर 2008 में मुंबई हमले के दौरान क?ई न्यूज चैनल्स के हमले के लाइव कवरेज का आतंकियों ने फायदा उठाया था। टेलीविजन न्यूज चैनल्स केवल देश के अंदरूनी मामलों में ही पक्षपाती बहस और खबरें नहीं प्रसारित कर रहे हैं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में भी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रही है। मीडिया का बुनियादी दायित्व युद्ध,आपदा, महामारी और अशांति में समाज में शांति और साकारात्मकता कायम करना है लेकिन टेलीविजन न्यूज चैनल्स अपने इन दायित्वों के प्रति हर विभिषिका में गैर जिम्मेदाराना रवैया ही अपनाता रहा है। पाठकों को स्मरण में होगा कि न्यूज़ चैनलों ने रुस-यूक्रेन युद्ध के शुरूआत में अपने स्टुडियो को युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया था और पूर्व सैन्य प्रमुखों तथा रक्षा विशेषज्ञों को बिठाकर बेफजूल की बहस प्रसारित कर रहे थे।तब इन टीवी चैनल्स के एंकर और स्टुडियो में मौजूद सैन्य विशेषज्ञू ने तीसरे विश्वयुद्ध शुरू होने की बकायदा समय भी तय कर चुके थे। विभिन्न नेशनल न्यूज चैनल्स लगातार इस युद्ध की विभीषिका की लाइव तस्वीरें दिखाते रहे जिसने दर्शकों के दिमाग में गहरा असर डाला। कोरोना महामारी के दौरान कतिपय न्यूज चैनलों ने देश में भय, दहशत, आक्रोश और धार्मिक वैमनस्यता परोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत में महामारी के शुरूआत में पहले देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के पैदल घर वापसी की लाइव समाचार प्रसारित कर देश में अफरातफरी और दहशत कायम करने में लगे रहे। न्यूज़ चैनलों ने देश में कोरोना के शुरूआती संक्रमण के लिए दिल्ली में तबलीगी जमात के धार्मिक आयोजन को जिम्मेदार मानते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को कठघरे में खड़ा करने और इस समुदाय द्वारा मेडिकल टीम के साथ पथराव और दुर्व्यवहार की खबरों को लगातार चलाया फलस्वरूप देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ। महामारी के दूसरी लहर के दौरान न्यूज चैनलों ने देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन और बिस्तर की कमी के कारण अस्पतालों के बाहर गलियारों और आटोरिक्शा में दम तोड़ते लोगों और रोते- बिलखते परिजनों की लगातार खबरें प्रसारित कर एक बड़ी आबादी में बेचैनी और डर पैदा कर दिया। बहरहाल टीवी चैनल्स अभी भी चीन में कोरोना महामारी के दहशत भरे खबरें चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं।
निराशाजनक यह कि कतिपय टीवी चैनल टीआरपी की होड़ में सनसनीखेज कार्यक्रम प्रसारित कर मीडिया के लिए जरूरी अनुशासन और
जवाबदेही की पाबंदियां लगातार लांघ रहे हैं। यहां यह भी विचारणीय है कि है कि अदालतों और सरकार ने जब -जब मीडिया की निरंकुशता पर अंकुश लगाने की कोशिश की तब-तब मानवाधिकार संगठनों और कथित बुद्धिजीवियों ने इसे बोलने की आजादी पर हमला बताते हुए हल्ला मचाया। बहरहाल अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर टीवी न्यूज चैनल्स द्वारा प्रसारित किए जा रहे ‘हेट स्पीच’ को किसी भी लिहाज से स्वीकार नहीं किया जा सकता लिहाजा ऐसे मनमानी पर अंकुश लगाना आवश्यक है।अभिव्यक्ति की आजादी की पैरवी करने वालों को यह बात जेहन में रखना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) ए के तहत प्राप्त बोलने की आजादी अनियंत्रित नहीं है बल्कि उस पर भी कानूनी पाबंदियां हैं। विचारणीय है कि मीडिया यानि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है यदि यही आधार देश के सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने लगे तो यह निश्चित ही चिंताजनक है। बहरहाल हर समस्या का समाधान केवल अदालतों के भरोसे संभव नहीं है बल्कि इसके लिए सरकार और मीडिया जगत को भी सामने आना होगा। महात्मा गांधी का मानना था कि कलम की निरंकुशता खतरनाक हो सकती है लेकिन उस व्यवस्था पर अंकुश और ज्यादा खतरनाक हो सकती है लिहाजा वे पत्रकारिता में स्व-नियमन और स्व-अनुशासन के पक्षधर थे।उक्त के मद्देनजर टीवी चैनलों और एंकरों को खुद अपने लिए एक लक्ष्मण रेखा तय करनी चाहिए ताकि पत्रकारिता की आत्मा जिंदा रहे आखिरकार यह जवाबदेही भी उनकी ही है।
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
आजकल हम भारतीय लोग इस बात से बहुत खुश होते रहते हैं कि भारत शीघ्र ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लेकिन दुनिया के इस तीसरे सबसे बड़े मालदार देश की असली हालत क्या है? इस देश में गरीबी भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है, जितनी तेजी से अमीरी बढ़ रही है। अमीर होनेवालों की संख्या सिर्फ सैकड़ों में होती है लेकिन गरीब होनेवालों की संख्या करोड़ों में होती है। आॅक्सफाॅम के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले दो साल में सिर्फ 64 अरबपति बढ़े हैं। सिर्फ 100 भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 54.12 लाख करोड़ रु. है याने उनके पास इतना पैसा है कि वह भारत सरकार के डेढ़ साल के बजट से भी ज्यादा है।
सारे अरबपतियों की संपत्ति पर मुश्किल से 2 प्रतिशत टैक्स लगता है। इस पैसे से देश के सारे भूखे लोगों को अगले तीन साल तक भोजन करवाया जा सकता है। यदि इन मालदारों पर थोड़ा ज्यादा टैक्स लगाया जाए और उपभोक्ता वस्तुओं का टैक्स घटा दिया जाए तो सबसे ज्यादा फायदा देश के गरीब लोगों को ही होगा। अभी तो देश में जितनी भी संपदा पैदा होती है, उसका 40 प्रतिशत सिर्फ 1 प्रतिशत लोग हजम कर जाते हैं जबकि 50 प्रतिशत लोगों को उसका 3 प्रतिशत हिस्सा ही हाथ लगता है। अमीर लोग अपने घरों में चार-चार कारें रखते हैं और गरीबों को खाने के लिए चार रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती। ये जो 50 प्रतिशत लोग हैं, इनसे सरकार जीएसटी का कुल 64 प्रतिशत पैसा वसूलती है जबकि देश के 10 प्रतिशत सबसे मालदार लोग सिर्फ 3 प्रतिशत टैक्स देते हैं।
इन 10 प्रतिशत लोगों के मुकाबले निचले 50 प्रतिशत लोग 6 गुना टैक्स भरते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को अपनी रोजमर्रा के जरूरी चीजों को खरीदने पर बहुत ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है, क्योंकि वह बताए बिना ही चुपचाप काट लिया जाता है। इसी का नतीजा है कि देश के 70 करोड़ लोगों की कुल संपत्ति देश के सिर्फ 21 अरबपतियों से भी कम है। साल भर में उनकी संपत्तियों में 121 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। अब जो नया बजट आनेवाला है, शायद सरकार इन ताजा आंकड़ों पर ध्यान देगी और भारत की टैक्स-व्यवस्था में जरुर कुछ सुधार करेगी। देश कितना ही मालदार हो जाए लेकिन यदि उसमें गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती गई तो वह संपन्नता किसी भी दिन हमारे लोकतंत्र को परलोकतंत्र में बदल सकती है। यह हमने पिछली दो सदियों में फ्रांस, रूस और चीन में होते हुए देखा है। (नया इंडिया की अनुमति से)
-जे. सुशील
‘बहुत साल पहले पोलैंड के एक लेखक हुए जोसेफ कोनराड। कोनराड पोलिश थे तो उन्होंने अंग्रेजी देर से सीखी लेकिन तय किया कि अंग्रेजी में ही लिखेंगे। कहते हैं कि बाईस साल में उन्होंने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया था। लेखन के अलावा वो दुनिया के अलग अलग जगहों (खास कर अफ्रीका) में बहुत लंबे समय तक रहे और ब्रितानी जहाजों पर ही यात्राएं कीं। उनकी किताबें इन यात्राओं से जुड़ी हुई हैं। जिसमें से एक किताब को बेहतरीन किताब माना गया- हार्ट ऑफ डार्कनेस। यह कांगो की यात्रा पर थी। जैसा कि नाम से जाहिर है यह एक आपत्तिजनक किताब होनी चाहिए थी लेकिन चूंकि वो समय साम्राज्यवाद का था तो किसी ने कुछ कहा नहीं। यह किताब मकबूल हुई इतनी कि ब्रितानी न होने के बावजूद अंग्रेजी साहित्य के कैनन में यह शामिल हो गई।
हालांकि इस किताब में साम्राज्यवाद की भी आलोचना है लेकिन उसमें अफ्रीकी लोगों का जो डेपिक्शन है वो बहुत खराब है। दुनिया के सभी अंग्रेजी के क्लासेस में ये पढ़ाई जाती रही। बीसवीं सदी में चालीस से लेकर साठ के दशक में एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद को उखाड़ फेंका गया। पचास के दशक में चिनुआ अचेबे, साठ के दशक में न्गूगी वा थियोंगो ने जो उपन्यास लिखे उनकी पृष्ठभूमि में हार्ट ऑफ डार्कनेस के बरक्स एक नैरेटिव खड़ा करना ही था।
जब लोग (फेसबुक पर तो बिना क्रेडिट दिए) इस वाक्य को कोट करते हैं कि जब तक शेर का इतिहास लिखने वाला कोई नहीं होगा तब तक शिकारी की वीरता के किस्से ही लोग सुनेंगे। (मूल कोट- until the lions have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunter) उन्हें ये नहीं पता होगा कि इस वाक्य की पृष्ठभूमि क्या है। अचेबे ने अपने इंटरव्यूज में यह स्पष्ट किया है कि जब वो कॉलेज में कोनराड की किताब पढ़ रहे थे तो वो इस बात से बहुत दुखी हुए थे और नाराज़ कि इस किताब में अफ्रीका के लोगों को किस तरह से दिखाया गया है।
वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपना उपन्यास लिखा भी इसी कारण से था। थिंग्स फॉल अपार्ट एक कालजयी उपन्यास है इसमें कोई शक नहीं रहा। आगे चलकर एडवर्ड सईद ने भी जोसेफ कोनराड पर ही पीएचडी की और सत्तर के दशक में उनकी किताब ओरिएन्टलिज़्म में भी कोनराड की इस किताब की गंभीर आलोचना है और कहा गया है कि कोनराड की दृष्टि में साम्राज्यवाद खराब तो था लेकिन उनके मन में अफ्रीकी लोगों के प्रति दुर्भाव भी स्पष्ट दिखता है। लेकिन यह लिखते हुए सईद कहीं भी यह नहीं कहते कि कोनराड घटिया आदमी थे या वो घटिया लेखक थे। सईद कहते हैं कि आदमी आलोचना उसी चीज की करता है जिससे वो बहुत प्रेम करता है। आप जिस टेक्सट से प्रेम में होंगे उसी की आलोचना करेंगे और यह ठीक भी है। किसी टेक्सट से घृणा कर के उसकी आलोचना नहीं हो सकती है।
साठ और सत्तर के दशक में कोनराड को रिडिफाईन किया गया। अस्सी के दशक में इस संदर्भ में चिनुआ अचेबे का एक अभूतपूर्व लेख है एन इमेज ऑफ अफ्रीका के नाम से। यह एक भाषण था जो उन्होंने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में दिया था जो बाद में मैसाचुसेट्स रिव्यू में छपा। इस लेख का पूरा टाइटल बहुत मजेदार है- 'An Image of Africa: Racism in Conrad's 'Heart of Darkness'
स्पष्ट है कि वो क्या चिन्हित कर रहे हैं लेकिन पूरे लेख में वो कहीं भी कोनराड पर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं कर रहे हैं। उनकी नस्ल पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं लेकिन उस लेख में जो आलोचना की गई है उससे कोई असहमत भी नहीं हो सकता है।
अब सवाल यह है- अगर कोनराड का लेखन नस्लभेदी था जो बहुत हद तक प्रमाणित है तो क्या कोनराड को पढ़ाया जाना बंद कर दिया गया यूनिवर्सिटियों में? नहीं। कोनराड अब भी पढ़ाए जाते हैं बस उसका संदर्भ बदल गया। अब ज्यादातर यूनिवर्सिटियों में उनकी किताब पढ़ाते हुए यह बताया जाता है कि कैसे उनके उपन्यास में अफ्रीकी लोगों को दर्शाया गया है जो प्रॉब्लमैटिक है। कई बार बहस में ग्रेजुएशन के बच्चे कहते हैं- कोनराड रेसिस्ट हैं जिस पर प्रोफेसर उन्हें टोकते हैं और कहते हैं हो सकता है वो रेसिस्ट हों लेकिन हमें उनके टेक्सट पर बात करनी चाहिए और बेहतर होगा ये कहना कि उनके टेक्सट में रेसिज्म दिखता है।
लेकिन ये महीन बात है। लोगों को इतना धैर्य नहीं है। तुलसीदास को बिना पढ़े उनके लिखे में से चार-पांच-दस लाइनें निकाल कर उन्हें जातिवादी, स्त्रीद्वेषी और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। किसी भी टेक्स्ट को उसके टाइम और स्पेस में भी देखा जाना चाहिए। यह कहा ही जा सकता है कि तुलसीदास के टेक्सट में स्त्रीद्वेषी पंक्तियां हैं लेकिन क्या इन पंक्तियों से उनके लेखन को खारिज किया जा सकता है पूरी तरह।
क्या ये बात याद नहीं रखी जानी चाहिए कि संस्कृत के प्रभुत्व के समय में वो अवधी में लिख रहे थे तो उन्हें उच्च वर्ग के लोगों से तिरस्कार मिला था। चीजों को संदर्भ में देखना समझना चाहिए। आलोचना तो होनी ही चाहिए इसमें क्या शक है लेकिन सुदीर्घ आलोचना हो। ये मैं कुछ अधिक उम्मीद कर रहा हूं शायद।
फेसबुक के जमाने में कथित पढ़े-लिखे लोग भी चार लाइन में तुलसी को निपटा कर आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि फिर कल सूर्यकुमार यादव करना है परसों मीडिया पर भाषण देना है नरसों किसी और को गरियाना है।
खैर। इस पोस्ट पर अब कोई मुझे भी ब्राम्हणवादी घोषित करेगा। ऐसा मैं अनुभव से कह रहा हूं। यह सामान्य है फेसबुक पर।’
‘तुलसीदास अवधी के महाकवि थे। विचारधारा उनकी वर्णव्यवस्था के पक्ष में थी। लेकिन माक्र्सवादी साहित्य चिंतन ने मुझे छात्र जीवन में ही सिखा दिया था, और नामवर सिंह के व्याख्यानों ने यह समझने में मदद की थी, कि किसी लेखक की विचारधारा उसकी विश्वदृष्टि का एक अवयव होती है। महत्वपूर्ण उसकी समूची विश्वदृष्टि है जिसके आलोक में उसके कृतित्व को समझा जाना चाहिए। आजकल खारिज करने का फैशन चल पड़ा है । कोई नागार्जुन को खारिज कर रहा है तो कोई तुलसी और निराला को। प्रेमचंद को तो सतीसमर्थक तक बताया जा चुका है। मेरा तो सिर्फ यह कहना है। अगर किसी लेखक को नहीं पढऩा चाहते हो तो न पढ़ो। प्रेमचंद को या निराला को या तुलसी-सूर को नहीं पढ़ोगे तो इनका तो कोई नुकसान होने वाला है नहीं। तुम्हारा ही होगा। और हाँ, जो कबीर इतने फैशन में हैं, नारी पर उनके विचार भी पढ़ लेना । ’ -कुलदीप कुमार
‘मैं किसी पुस्तक को जलाने के पक्ष में नहीं हूं, वह मनुस्मृति हो या ‘बंचेज आप थाट्स’ हो। पढ़ सकें तो पढिय़े, गुनिये-समझिये और बढिय़ा बहस कीजिए। तर्क से खारिज करना पुस्तक जलाने से अधिक प्रभावशाली होगा। तर्क के धनी हैं तो ‘जला दो, मिटा दो’ वाला नकारात्मक रास्ता क्यों चुन रहे हैं? यदि पुस्तक जलाने की संस्कृति सही है तो केवल मनुस्मृति और रामचरितमानस जलाने तक ही यह अभियान नहीं रुकेगा, कल को ‘एनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ और ‘दास कैपिटल’ भी इसकी जद में आ सकते हैं।’ ‘प्रेमचंद की रचनावली (जनवाणी प्रकाशन, दिल्ली) में संकलित, प्रेमचंद की ओर से उनकी बेटी के भावी ससुर को लिखे गये एक विवादास्पद पत्र, जो स्त्री की दृष्टि से अत्यंत आधुनिकता-विरोधी है, पर चली बहस में प्रेमचंद के पक्ष में हिंदी के प्रखर, प्रतिबद्ध और पाठकों के बीच बहुत पसंद किये जाने वाले आलोचक वीरेंद्र यादव ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी कि ‘ख्याल रहे, नहलाने के बाद बाथ-टब से केवल मैला पानी बहाना है। ऐसा न हो कि पानी के साथ बेबी को भी बहा दें।’ मुझे लगता है तुलसीदास पर बात करते हुए भी उनकी यह बात हमें याद रखनी चाहिए।’
-सूर्य नारायण (प्रोफेसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय)
अशोक पांडे
मशीनों ने दलाई लामा को बचपन से ही आकर्षित किया। पोटाला महल में जो भी मशीन दिखाई देती, पेंचकस वगैरह लेकर उसके उर्जे-पुर्जे खोलकर अलग करना और उन्हें फिर से जोडऩे का खेल उन्हें पसंद था। ल्हासा में तब कुल तीन कारें थीं। तीनों उन्हीं की थीं। उन्होंने इन कारों को भी कई दफा खोला-जोड़ा।
ऑस्ट्रियाई पर्वतारोही हाइनरिख हैरर एक बेहद मुश्किल और दुस्साहस-भरे अभियान के बाद 1946 में जब तिब्बत पहुंचे तो उनकी मुलाकात किशोर दलाई लामा से हुई। यह मुलाकात एक बेहद अन्तरंग मित्रता में तब्दील हुई और 2006 में हुए हैरर के देहांत तक बनी रही। हैरर ने तिब्बत के अपने अनुभवों को ‘सेवेन ईयर्स इन तिब्बत’ के नाम से प्रकाशित किया। इस बेस्टसेलर पर इसी नाम से फिल्म भी बनी है।
हाइनरिख हैरर और दलाई लामा के बीच पच्चीस साल का फासला था। दोनों की जन्मतिथि इत्तफाकन एक ही थी-6 जुलाई। किशोर दलाई लामा के लिए हैरर एक ऐसी खिडक़ी बन गए जिसकी मदद से आधुनिक संसार को देखा-समझा जा सकता था। हैरर को तिब्बत सरकार में बाकायदा नौकरी दी गई और बहुत सारे महत्वपूर्ण काम सौंपे गए। उन्हें विदेशी समाचारों का अनुवाद करना होता था, महत्वपूर्ण अवसरों के फोटो खींचने होते थे और दलाई लामा को ट्यूशन पढ़ाना होता था। इस तरह खेल-विज्ञान के ग्रेजुएट हाइनरिख हैरर तिब्बत के किशोर धर्मगुरु के अंग्रेज़ी, भूगोल और विज्ञान अध्यापक बने। हैरर ने दलाई लामा के लिए स्केटिंग रिंक तैयार करने के अलावा एक सिनेमा हॉल भी बनाया जिसके प्रोजेक्टर को जीप इंजिन की सहायता से चलाया जाता था।
उधर अमेरिका किसी तरह भारत के रास्ते चीन तक सडक़ बनाने के मंसूबे देख रहा था। तिब्बत से होकर जाने वाले रास्ते में उसे संभावना दिखाई दी तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपने दो प्रतिनिधियों को ल्हासा भेजा। प्रसंगवश इन दो में से एक आदमी रूसी मूल का था जिसका नाम इल्या था और वह लियो टॉलस्टॉय का पोता था। रूजवेल्ट ने बालक दलाई लामा के लिए एक विशेष उपहार भेजा। जेनेवा की मशहूर घड़ीसाज़ कम्पनी पाटेक फिलिप ने उस एक्सक्लूसिव मॉडल की 1937 और 1950 के बीच कुल 15 घडिय़ाँ बनाई थीं। ऐसी एक घड़ी 2014 में पांच लाख डॉलर में नीलाम हुई थी।
बहरहाल पोटाला महल की एक-एक घड़ी के अस्थि-पंजर ढीले कर चुके दलाई लामा ने इस घड़ी के साथ भी वही सुलूक किया। हैरर की संगत में अब वे एक एक्सपर्ट बन चुके थे। उसके बाद से पुरानी घडिय़ों को इकठ्ठा करना और उनकी मरम्मत करना दलाई लामा का सबसे बड़ा शौक है।
चीन के दुष्ट साम्राज्यवादी मंसूबों के कारण उन्हें अपना देश छोडऩा पड़ा। उनका तिब्बत आज भी बीसवीं शताब्दी में मानवीय विस्थापन की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है।
दुनिया भर में फैले अपने अनुयायियों के बीच भगवान की हैसियत रखने वाले, संसार की सबसे मीठी हंसी के स्वामी दलाई लामा को दुनिया भर के मसले निबटाने के बाद आज भी फुर्सत मिलती है तो वे घडिय़ाँ ठीक करते हैं। कभी-कभी इनमें बेहद आम लोगों की घडिय़ाँ भी होती हैं।
‘अगर मैं भिक्षु नहीं बनता तो मुझे पक्का इंजीनियर बनना था’ वे अक्सर कहते हैं।






.jpeg)